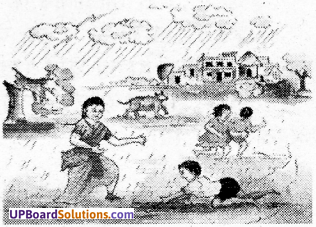UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi नाटक Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी) are part of UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi . Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi नाटक Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी).
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 11 |
| Subject |
Sahityik Hindi |
| Chapter |
Chapter 4 |
| Chapter Name |
सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी) |
| Number of Questions |
17 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi नाटक Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी)
प्रश्न 1:
‘सूत-पुत्र’ नाटक का कथा-सार संक्षेप में लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की कथावस्तु लिखिए।
उत्तर:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के लेखक डॉ० गंगासहाय प्रेमी हैं। इस नाटक के कथासूत्र ‘महाभारत’ से लिये गये हैं। परशुराम जी उत्तराखण्ड के आश्रम में निवास करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह केवल ब्राह्मणों को ही धनुष चलाना सिखाएँगे, क्षत्रियों को नहीं। ‘कर्ण’ एक महान् धनुर्धर बनना चाहते हैं; अतः वे स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने लगते हैं। एक दिन परशुराम जी, कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोये हुए होते हैं कि एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर कोटने लगता है, जिससे रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव होने पर भी ‘कर्ण’ दर्द सहन कर जाते हैं। कर्ण की सहनशीलता को देखकर परशुराम जी को उसके क्षत्रिय होने का सन्देह होता है। पूछने पर कर्ण उन्हें सत्य बता देते हैं। परशुराम जी क्रुद्ध होकर शाप देते हैं कि अन्त समय में तुम हमारे द्वारा सिखाई गयी विद्या को भूल जाओगे। कर्ण वहाँ से वापस चले आते हैं।
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत सूत-पुत्र’ नाटक के दूसरे अंक में द्रौपदी के विवाह का वर्णन है। पांचाल-नरेश द्रुपद के यहाँ उनकी अद्वितीया सुन्दरी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होता है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार प्रतिभागी को खौलते तेल की कड़ाही में ऊपर लगे खम्बे पर एक घूमते चक्र में बंधी मछली की आँख बेधनी थी। अनेक राजकुमार इसमें असफल हो जाते हैं। कर्ण अपनी विद्या पर विश्वास कर मछली की आँख बेधने आते हैं, लेकिन अपने परिचय से राजा द्रुपद को सन्तुष्ट नहीं कर पाते और द्रुपद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं।
कर्ण के तेजस्वी रूप तथा विद्रोही स्वभाव से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उसे अपने राज्य के एक प्रदेश ‘अंग देश’ का राजा घोषित कर दिया, किन्तु ऐसा करके भी दुर्योधन, कर्ण की पात्रता और क्षत्रियत्व को पुष्ट नहीं कर पाता। यह प्रसंग ही दुर्योधन व कर्ण की मित्रता का सेतु सिद्ध होता है। ब्राह्मण वेश में अर्जुन और भम सभा-मण्डप में आते हैं। अर्जुन मछली की आँख बेधकर द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। अर्जुन तथा भीम को दुर्योधन पहचान लेता है। दुर्योधन द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने के लिए कर्ण से कहता है, परन्तु कर्ण इसे अनैतिक कार्य के लिए तैयार नहीं होते। दुर्योधन अर्जुन से संघर्ष करता है, परन्तु घायल होकर वापस आ जाता है और कर्ण को बताता है कि ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं अर्जुन और भीम ही हैं। इस बात में भी कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि पाण्डवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की उसकी योजना असफल हो गयी है। कर्ण पाण्डवों को बड़ा भाग्यशाली बताता है।
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक के तीसरे अंक में कर्ण के तपोस्थान का वर्णन है। कर्ण सूर्य भगवान् की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान् साक्षात् दर्शन देकर उसे कवच तथा कुण्डल देते हैं और उनके जन्म का सारा रहस्य उन्हें बताते हैं। साथ ही आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये कवच-कुण्डल तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, तब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। सूर्य भगवान् कर्ण को आगामी भारी संकटों से सचेत करते हैं और कहते हैं कि इन्द्र तुमसे इन कवच और कुण्डल की माँग करेंगे। कर्ण के पिछले जीवन की कथा भी सूर्य भगवान् उन्हें बता देते हैं, लेकिन माता का नाम नहीं बताते। कुछ समय बाद इन्द्र; अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में आकर दानवीर कर्ण से कवच व कुण्डल का दान ले लेते हैं। कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर वे उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इन्द्र कर्ण को यह रहस्य भी बता देते हैं कि कुन्ती से, सूर्य के द्वारा, कुमारी अवस्था में उनका जन्म हुआ है। इस जानकारी के कुछ समय बाद कुन्ती कर्ण के आश्रम में आती है और कर्ण को बताती है कि वे उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह कर्ण से रणभूमि में पाण्डवों को न मारने का वचन चाहती है; परन्तु कर्ण ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वे कुन्ती को आश्वासन देते हैं कि वे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पाण्डव को नहीं मारेंगे। कुन्ती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है। नाटक का तीसरा अंक यहीं समाप्त हो जाता है।
डॉ० गंगासहाय प्रेमी द्वारा रचित ‘सूर्त-पुत्र’ नाटक के चौथे (अन्तिम) अंक में अर्जुन तथा कर्ण के युद्ध का वर्णन है। यह अंक नाटक का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावित करने वाला अंक है। इसमें नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, बाहुबल और दृढ़प्रतिज्ञता जैसे गुणों का उद्घाटन हुआ है। कर्ण और अर्जुन को युद्ध होता है। कर्ण अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन के रथ को युद्ध-क्षेत्र में पीछे हटा देते हैं। कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं, जो अर्जुन को अच्छी नहीं लगती। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारी पताका पर ‘महावीर’, रथ के पहियों पर ‘शेषनाग और तीनों लोकों का भार लिये मैं रथ पर स्वयं प्रस्तुत हुँ, फिर भी कर्ण ने रथ को पीछे हटा दिया, निश्चय ही वह प्रशंसा का पात्र है। युद्धस्थल में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फँस जाता है। अर्जुन निहत्थे कर्ण को बाण-वर्षा करके घायल कर देते हैं। कर्ण मर्मान्तक रूप से घायल हो गिर पड़ते हैं और सन्ध्या हो जाने के कारण युद्ध बन्द हो जाता है। श्रीकृष्ण कर्ण की दानवीरता एवं प्रतिज्ञा-पालन की प्रशंसा करते हैं। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए श्रीकृष्ण व अर्जुन घायल कर्ण के पास सोने का दान माँगने जाते हैं। कर्ण उन्हें । अपने सोने के दाँत तोड़कर देता है, परन्तु रक्त लगा होने के कारण अशुद्ध बताकर कृष्ण उन्हें लेना स्वीकार नहीं करते। तब रक्त लगे दाँतों की शुद्धि के लिए कर्ण बाण मारकर धरती से जल निकालता है और दाँतों को धोकर ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण को दे देता है। अब श्रीकृष्ण और अर्जुन वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्रीकृष्ण कर्ण से लिपट जाते हैं और अर्जुन कर्ण के चरण पकड़ लेते हैं। यहीं पर ‘सूत-पुत्र’ नाटक की कथा का मार्मिक व अविस्मरणीय अन्त होता है।
प्रश्न 2:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के प्रथम अंक की कथा को संक्षेप में लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के किसी एक अंक की कथा पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के लेखक डॉ० गंगासहाय प्रेमी हैं। इस नाटक के कथासूत्र ‘महाभारत’ से लिये गये हैं। परशुराम जी उत्तराखण्ड के आश्रम में निवास करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह केवल ब्राह्मणों को ही धनुष चलाना सिखाएँगे, क्षत्रियों को नहीं। ‘कर्ण’ एक महान् धनुर्धर बनना चाहते हैं; अतः वे स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने लगते हैं। एक दिन परशुराम जी, कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोये हुए होते हैं कि एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर कोटने लगता है, जिससे रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव होने पर भी ‘कर्ण’ दर्द सहन कर जाते हैं। कर्ण की सहनशीलता को देखकर परशुराम जी को उसके क्षत्रिय होने का सन्देह होता है। पूछने पर कर्ण उन्हें सत्य बता देते हैं। परशुराम जी क्रुद्ध होकर शाप देते हैं कि अन्त समय में तुम हमारे द्वारा सिखाई गयी विद्या को भूल जाओगे। कर्ण वहाँ से वापस चले आते हैं।
प्रश्न 3:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के द्वितीय अंक की कथा का सार संक्षेप में लिखिए।
या
द्रौपदी स्वयंवर की कथा ‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर द्रौपदी-स्वयंवर में कर्ण का जो अपमान हुआ उस पर प्रकाश डालिए।
या
कर्ण और दुर्योधन में मित्रता किस प्रकार हुई ? ‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर बताइट।
या
“द्रौपदी स्वयंवर’ का कथानक अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत सूत-पुत्र’ नाटक के दूसरे अंक में द्रौपदी के विवाह का वर्णन है। पांचाल-नरेश द्रुपद के यहाँ उनकी अद्वितीया सुन्दरी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होता है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार प्रतिभागी को खौलते तेल की कड़ाही में ऊपर लगे खम्बे पर एक घूमते चक्र में बंधी मछली की आँख बेधनी थी। अनेक राजकुमार इसमें असफल हो जाते हैं। कर्ण अपनी विद्या पर विश्वास कर मछली की आँख बेधने आते हैं, लेकिन अपने परिचय से राजा द्रुपद को सन्तुष्ट नहीं कर पाते और द्रुपद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं।
कर्ण के तेजस्वी रूप तथा विद्रोही स्वभाव से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उसे अपने राज्य के एक प्रदेश ‘अंग देश’ का राजा घोषित कर दिया, किन्तु ऐसा करके भी दुर्योधन, कर्ण की पात्रता और क्षत्रियत्व को पुष्ट नहीं कर पाता। यह प्रसंग ही दुर्योधन व कर्ण की मित्रता का सेतु सिद्ध होता है। ब्राह्मण वेश में अर्जुन और भम सभा-मण्डप में आते हैं। अर्जुन मछली की आँख बेधकर द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। अर्जुन तथा भीम को दुर्योधन पहचान लेता है। दुर्योधन द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने के लिए कर्ण से कहता है, परन्तु कर्ण इसे अनैतिक कार्य के लिए तैयार नहीं होते। दुर्योधन अर्जुन से संघर्ष करता है, परन्तु घायल होकर वापस आ जाता है और कर्ण को बताता है कि ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं अर्जुन और भीम ही हैं। इस बात में भी कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि पाण्डवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की उसकी योजना असफल हो गयी है। कर्ण पाण्डवों को बड़ा भाग्यशाली बताता है।
प्रश्न 4:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के तृतीय अंक की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के तृतीय अंक में कर्ण-इन्द्र अथवा कर्ण-कुन्ती संवाद का सारांश लिखिए।
या
सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर कर्ण के अन्तर्द्वन्द्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक के तीसरे अंक में कर्ण के तपोस्थान का वर्णन है। कर्ण सूर्य भगवान् की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान् साक्षात् दर्शन देकर उसे कवच तथा कुण्डल देते हैं और उनके जन्म का सारा रहस्य उन्हें बताते हैं। साथ ही आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये कवच-कुण्डल तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, तब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। सूर्य भगवान् कर्ण को आगामी भारी संकटों से सचेत करते हैं और कहते हैं कि इन्द्र तुमसे इन कवच और कुण्डल की माँग करेंगे। कर्ण के पिछले जीवन की कथा भी सूर्य भगवान् उन्हें बता देते हैं, लेकिन माता का नाम नहीं बताते। कुछ समय बाद इन्द्र; अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में आकर दानवीर कर्ण से कवच व कुण्डल का दान ले लेते हैं। कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर वे उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इन्द्र कर्ण को यह रहस्य भी बता देते हैं कि कुन्ती से, सूर्य के द्वारा, कुमारी अवस्था में उनका जन्म हुआ है। इस जानकारी के कुछ समय बाद कुन्ती कर्ण के आश्रम में आती है और कर्ण को बताती है कि वे उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह कर्ण से रणभूमि में पाण्डवों को न मारने का वचन चाहती है; परन्तु कर्ण ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वे कुन्ती को आश्वासन देते हैं कि वे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पाण्डव को नहीं मारेंगे। कुन्ती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है। नाटक का तीसरा अंक यहीं समाप्त हो जाता है।
प्रश्न 5:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के चतुर्थ अंक की समीक्षा कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के अन्तिम अंक की कथा संक्षेप में लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र के चतुर्थ अंक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कर्ण युद्धवीर होने के साथ-साथ दानवीर भी था।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी द्वारा रचित ‘सूर्त-पुत्र’ नाटक के चौथे (अन्तिम) अंक में अर्जुन तथा कर्ण के युद्ध का वर्णन है। यह अंक नाटक का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावित करने वाला अंक है। इसमें नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, बाहुबल और दृढ़प्रतिज्ञता जैसे गुणों का उद्घाटन हुआ है। कर्ण और अर्जुन को युद्ध होता है। कर्ण अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन के रथ को युद्ध-क्षेत्र में पीछे हटा देते हैं। कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं, जो अर्जुन को अच्छी नहीं लगती। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारी पताका पर ‘महावीर’, रथ के पहियों पर ‘शेषनाग और तीनों लोकों का भार लिये मैं रथ पर स्वयं प्रस्तुत हुँ, फिर भी कर्ण ने रथ को पीछे हटा दिया, निश्चय ही वह प्रशंसा का पात्र है। युद्धस्थल में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फँस जाता है। अर्जुन निहत्थे कर्ण को बाण-वर्षा करके घायल कर देते हैं। कर्ण मर्मान्तक रूप से घायल हो गिर पड़ते हैं और सन्ध्या हो जाने के कारण युद्ध बन्द हो जाता है। श्रीकृष्ण कर्ण की दानवीरता एवं प्रतिज्ञा-पालन की प्रशंसा करते हैं। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए श्रीकृष्ण व अर्जुन घायल कर्ण के पास सोने का दान माँगने जाते हैं। कर्ण उन्हें । अपने सोने के दाँत तोड़कर देता है, परन्तु रक्त लगा होने के कारण अशुद्ध बताकर कृष्ण उन्हें लेना स्वीकार नहीं करते। तब रक्त लगे दाँतों की शुद्धि के लिए कर्ण बाण मारकर धरती से जल निकालता है और दाँतों को धोकर ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण को दे देता है। अब श्रीकृष्ण और अर्जुन वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्रीकृष्ण कर्ण से लिपट जाते हैं और अर्जुन कर्ण के चरण पकड़ लेते हैं। यहीं पर ‘सूत-पुत्र’ नाटक की कथा का मार्मिक व अविस्मरणीय अन्त होता है।
प्रश्न 6:
नाट्य-कला की दृष्टि से ‘सूत-पुत्र की समीक्षा कीजिए।
या
अभिनय और रंगमंच की दृष्टि से ‘सूत-पुत्र की समीक्षा कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के उद्देश्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की संवाद-योजना की समीक्षा कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र की कथावस्तु की समीक्षा कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की भाषा-शैली की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की भाषा पर प्रकाश डालिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के देश-काल एवं वातावरण पर प्रकाश डालिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की मौलिक विशेषताएँ लिखिए।
‘सूत-पुत्र’ नाटक के नाट्य-शिल्प पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
‘सूत-पुत्र’ नाटक की तात्त्विक समीक्षा
नाट्य-कला की दृष्टि से डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक की तात्त्विक समीक्षा निम्नवत् है
(1) कथानक – यह ‘महाभारत की कथा से सम्बन्धित ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में दानवीर कर्ण के जीवनकाल की घटनाओं का वर्णन है। नाटक चार अंकों में विभाजित है। चौथे अंक में तीन दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं। कथा का आरम्भ कर्ण-परशुराम संवाद से तथा कथा का विकास परशुराम द्वारा कर्ण को आश्रम से निकालने की घटना के द्वारा होता है। इन्द्र द्वारा कवच-कुण्डल माँग लेने की घटना नाटक की चरम सीमा’ को प्रस्तुत करती है। कुन्ती-कर्ण संवाद के समय नाटक ‘उतार’ पर होता है तथा विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ कर्ण के सम्पूर्ण जीवनकाल की घटनाओं को प्रस्तुत करता है। कथानक सुसंगठित, लोक-प्रसिद्ध तथा घटनाप्रधान है। सभी अंक तथा दृश्य एक सूत्र में बँधे हैं।
कथानक यद्यपि महाभारतकालीन ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं पर आधारित है, किन्तु लेखक ने इसके माध्यम से वर्तमान समाज में व्याप्त जाति एवं वर्ण-व्यवस्था से सम्बद्ध विसंगतियों का भी परोक्ष प्रकाशन किया है। नारी-शिक्षा का अभाव, नारी की सामाजिक दयनीयता, समाज में नारियों की विवशता आदि का चित्रण वर्तमान विसंगतियों की ओर ही संकेत करती है।
(2) पात्र एवं चरित्र-चित्रण – लेखक ने ‘सूत-पुत्र’ नाटक के अधिकांश पात्रों का चयन ‘महाभारत’ से किया है। लेखक का मत है कि ‘महाभारत’ की घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। नाटक के प्रमुख पात्र कर्ण, श्रीकृष्ण, अर्जुन, परशुराम, दुर्योधन इत्यादि हैं। गौण पात्रों में भीम, कुन्ती, सूर्य, इन्द्र इत्यादि हैं। गौणातिगौण श्रेणी के अन्य पात्र भी हैं, जिनका उल्लेख-मात्र ही नाटक में है। यह सम्पूर्ण नाटक कर्ण के चरित्र को ही प्रकाशित करता है। अन्य पात्रों का चयन कर्ण के चरित्र की विशेषताओं को प्रकाशित करने एवं उसकी सामाजिक-मानसिक ताड़ना को स्वर देने के लिए किया गया है।
(3) संवाद-योजना ( कथोपकथन) – नाटक के संवाद पात्रानुकूल हैं। सरसता तथा भाव- अभिव्यंजना संवादों के अनन्य गुण हैं। नाटक में गीतों का प्रयोग भी हुआ है। स्वगत कथन अधिक हैं, जिससे कथा-प्रवाह में कुछ रुकावट आती है। संवाद-योजना की दृष्टि से नाटक श्रेष्ठ है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है
पहला स्वर-विशालकाय जी ! आप कड़ाह तक गये, यही बहुत है।
दूसरा स्वर-मोटे जी को कोई दुःख नहीं, अपनी असफलता का।।
कर्ण तथा परशुराम के कुछ स्वाभाविक संवादों के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं
परशुराम मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहता हूँ, जो तुमने मुझसे विद्या पढ़ने से पहले की थी। तुम मेरी सिखाई गयी विद्या किसी को सिखाओगे नहीं कर्ण!।
कर्ण – मुझे यह भली-भाँति स्मरण है गुरुदेव ! आप स्मरण न कराते, तब भी मैं उस प्रतिज्ञा का पालन करता।
प्रासंगिक कथाओं के चित्रण में वार्तालाप का सहारा लेकर नाटककार ने संवादों को लम्बा होने से बचा लिया। है। संवाद-योजना में नाटककार ने अपनी योग्यता, मौलिकता एवं कल्पना-शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। नाटक के संवादों में कहीं भी शिथिलता नहीं है।
(4) देश-काल और वातावरण – देश-काल और वातावरण की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक की पृष्ठभूमि पौराणिक है, परन्तु नाटककार ने नारी के स्थान को समाज में स्थापित करने के लिए आधुनिक परिवेश को भी प्रस्तुत किया है। वेशभूषा, युद्ध के उपकरण, स्वयंवर, धर्म इत्यादि की मान्यताओं की दृष्टि से ऐतिहासिक-पौराणिक वातावरण की संयोजना में लेखक को सफलता मिली है। परशुराम का आश्रम, द्रुपद-नरेश द्वारा आयोजित स्वयंवर-सभा, युद्धभूमि आदि को तत्कालीन वातावरण के अनुरूप सृजित करने में नाटककार ने सफलता प्राप्त की है।
(5) अभिनेयता अथवा रंगमंचीयता – अभिनेयता की दृष्टि से ‘सूत-पुत्र’ नाटक अधिक श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता। चार अंकों का मंचन कुछ अधिक लम्बा हो जाता है। फिर चौथे अंक में तो दृश्यों की संख्या भी तीन है। इस प्रकार मंच पर छह से अधिक सेट लगाने पड़ेंगे। पठनीयता की दृष्टि से नाटक उचित है।
(6) भाषा-शैली – नाटक की भाषा खड़ी बोली है और पात्रों के पूर्णतया अनुकूल है। संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग है। उर्दू, फारसी के शब्द अपेक्षाकृत कम हैं। चक्कर में पड़ना, अंगारे बरसना, फूलों की शय्या इत्यादि लोकोक्ति और मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से नाटक संवादात्मक तथा सम्भाषण-प्रधान है। स्वगत शैली तथा काव्य शैली का प्रयोग भी हुआ है। प्रसाद तथा ओज-गुण, शैली की विशेषता हैं। नाटक में वीर रस की प्रधानता है, अतः इसमें ओजगुण सर्वत्र द्रष्टव्य है। कहीं-कहीं हास्य-व्यंग्य का पुट भी परिलक्षित होता है। भाषा का एक उदाहरण द्रुपद नरेश के कथन में द्रष्टव्य है
“तब तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। ब्राह्मण का काम अकिंचन बनकर चल सकता है, पर क्षत्रिय को तो भूमि का स्वामी होना ही चाहिए। तुम साधारण व्यक्ति होकर मेरी कन्या से विवाह की कल्पना कैसे कर सके? यदि लक्ष्यवेध में सफल हो गये तो उसे खिलाओगे क्या? तुम स्वयं को साधारण व्यक्ति बता रहे हो। मेरे दास तक असाधारण धनी हैं। तुम अपने स्थान पर लौट जाओ।”
(7) उद्देश्य – इस नाटक का उद्देश्य आधुनिक समाज में जाति और धर्म की समस्या, विवाह पूर्व उत्पन्न सन्तान की समस्या इत्यादि का उद्घाटन करके इन समस्याओं के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करना है। कर्ण के दानवीर, युद्धवीर, गुरुभक्त तथा आदर्श मानवोचित उदात्त गुणों को प्रस्तुत करना भी नाटक का उद्देश्य है। नाटककार नाटक के माध्यम से वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा है।
प्रश्न 7:
सत-पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए
या
‘सूत-पुत्र के नायक कर्ण का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
‘महाभारत’ के सभी पात्रों पर कुछ-न-कुछ लांछन लगा हुआ है, पर कर्ण का चरित्र सभी प्रकार से उज्ज्वल है।” ‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कर्ण सभी प्रकार से महान था।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के नायक के चरित्र पक्ष की विवेचना कीजिए।
या
‘सूत्र-पुत्र’ नाटक के प्रमुख पात्र की विशेषताएँ लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र के प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है ?
या
कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र-चित्रण संक्षेप में कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के पुरुष पात्रों में आपको कौन-सा पात्र प्रिय है और क्यों ? तर्कसहित उत्तर दीजिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी के सूत-पुत्र’ नाटक का नायक कर्ण है। कर्ण के महान् चरित्र को प्रस्तुत कर उसकी महानता का सन्देश देना ही नाटककार का अभीष्ट है। कर्ण का जन्म कुन्ती द्वारा कौमार्य अवस्था में किये गये सूर्यदेव के आह्वान का परिणाम था। लोकलाज के भय से उसने कर्ण को एक घड़े में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहीं से कर्ण सूत-पत्नी राधा को मिला तथा राधा ने ही उसका पालन-पोषण किया। राधा द्वारा पालन-पोषण किये जाने के कारण कर्ण राधेय’ या ‘सूत-पुत्र’ कहलाया। असवर्ण परिवार में पालन-पोषण होने के कारण उसे पग-पग पर अपमान सहना पड़ा। अन्यायी और दुराचारी दुर्योधन की मित्रता भी उसकी असफलता का कारण बनी; क्योंकि मित्रता निभाने के लिए उसे अन्याय में भी उसका साथ देना पड़ा और अन्याय की अन्त में पराजय होती है तथा अन्यायी का साथ देने वाला भी बच नहीं पाता। कर्ण वीर, साहसी, दानवीर, क्षमाशील, उदार, बलशाली तथा सुन्दर था। यह सब होते हुए भी पग-पग पर अपमानित होने के कारण वह आजीवन तिल-तिल कर जलता रहा। उसका जीवन फूलों की शय्या नहीं, वरन् काँटों का बिछौना ही रहा।
कर्ण का चरित्र-चित्रण
कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं
(1) सुन्दर आकर्षक युवक – नाटककार ने कर्ण के रूप के विषय में लिखा है-“कर्ण तीस-पैंतीस वर्ष का हृष्ट-पुष्ट सुदर्शन युवा है। उसका शरीर लम्बा-छरहरा किन्तु भरा हुआ, रंग उज्ज्वल, गोरा, नाक ऊँची, नुकीली और आँखें बड़ी-बड़ी हैं।” इस प्रकार कर्ण एक सुन्दर आकर्षक युवक है।
(2) तेजस्वी तथा प्रतिभाशाली – कर्ण का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली है। वह अपने पिता सूर्य के समान तेजस्वी है। कर्ण ऐसा पहला व्यक्ति है, जिसके तेजस्वी रूप से दुर्योधनं जैसा अभिमानी व्यक्ति भी द्रौपदी-स्वयंवर में पहली बार देखकर ही प्रभावित होता है और अपना मित्र बनाने के लिए वह उसे अंगदेश का अधिपति बना देता है।
(3) सच्चा गुरुभक्त – कर्ण गुरुभक्त शिष्य है। गुरु परशुराम उसकी जंघा पर सिर रखकर सोते हैं, तभी एक कीड़ा उसकी जंघा को काटने लगता है। कीड़े के काटने पर उसकी जंघा से रक्तस्राव होता रहा, परन्तु कष्ट सहकर भी वह गुरु-निद्रा भंग नहीं होने देता। यद्यपि गुरु उसे शाप देते हैं, फिर भी वह किसी से उनकी निन्दा नहीं सुन सकता- “मेरे गुरु की निन्दा में अपने अब यदि एक भी शब्द कहा तो यह स्वयंवर-मण्डप युद्धस्थल में बदल जाएगा।” गुरु में कर्ण की अटूट श्रद्धा और भक्ति है। कर्ण की गुरु-भक्ति की प्रशंसा स्वयं गुरु परशुराम भी करते हैं-‘विद्याभ्यास के प्रति तुम्हारी तन्मयता से मैं सदा प्रभावित रहा हूँ। मेरे लिए तुम प्राण भी दे सकते हो।’
(4) धनुर्विद्या में प्रवीण – कर्ण ने धनुष चलाने की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। कर्ण अपने समय का सर्वश्रेष्ठ बाण चलाने वाला है। अनुपम धनुर्धारी अर्जुन भी उसे पराजित करने में समर्थ नहीं होता। साधारण योद्धाओं से युद्ध करना तो कर्ण अपनी शान के विरुद्ध समझता है।
(5) नारी के प्रति श्रद्धाभाव – कर्ण के प्रति सबसे बड़ा अन्याय स्वयं नारीस्वरूपा उसकी माँ ने किया है, परन्तु फिर भी वह नारी के प्रति श्रद्धाभाव रखता है “नारी विधाता का वरदान है। नारी सभ्यता, संस्कृति की प्रेरणा है। नारी का अपहरण कभी भी सह्य नहीं हो सकता।”
(6) दानवीर – कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानवीरता है। उसके सामने से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। अपनी रक्षा के अमोघ साधन कवच और कुण्डल भी वह इन्द्र के माँगने पर दान कर देता है। इस सम्बन्ध में अपने पिता सूर्य की सलाह भी वह नहीं मानता। वह इन्द्र से कहता है-“मुझे जितना कष्ट हो रहा है, उससे कई गुना सुख भी मिल रहा है।”
(7) विश्वासपात्र मित्र – वह एक सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाता है और कर्ण जीवन भर उसकी मित्रता का निर्वाह करता है। कुन्ती के कहने पर भी वह दुर्योधन से मित्रता के बन्धनों को तोड़कर विश्वासघाती नहीं बनना चाहता।
(8) प्रबल नैतिक – कर्ण उच्चकोटि के संस्कारों से युक्त है, अतः वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्त्व प्रदान करता है। द्रौपदी के अपहरण की बात पर वह दुर्योधन से कहता है- “दूसरे अनुचित करते हैं इसलिए हम भी अनुचित करें, यह नीति नहीं है। किसी की पत्नी का अपहरण परम्परा से निन्दनीय है।”
कुन्ती ने जब कर्ण से उसके जन्म की वास्तविकता बतायी और उसे अपने भाइयों के पास आ जाने के लिए कहा, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का यह कार्य नैतिकता से परिपूर्ण है। किसी व्यक्ति को आश्वासन देकर बीच में छोड़ना नैतिकता नहीं है। यदि भीष्म पितामह और कर्ण के व्यवहार को इस कसौटी पर परखें तो कर्ण को ही उत्तम कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह जहाँ परिस्थितियाँ न बदलने पर भी बदल गये वहाँ कर्ण परिस्थितियाँ बदलने पर भी नहीं बदला। कुन्ती ने कर्ण को ममता में फाँसने के साथ-साथ राज्य प्राप्ति का लालच भी दिया था, पर कर्ण सभी आकर्षणों से अप्रभावित रहा। जब कुन्ती ने बार-बार मातृत्व की दुहाई दी तो भी उसने युद्धस्थल में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पाण्डव का वध न करने की शपथ ली। जन्म एवं पालन-पोषण सम्बन्धी अपवाद के कारण कर्ण को चाहे जो कह लिया जाए, वैसे उसके चरित्र में कहीं भी कोई भी कालिमा नहीं है। कर्ण स्वनिर्मित व्यक्ति था। उसने किसी को न कभी धोखा दिया और न अकारण किसी से बैर-विरोध मोल लिया। महाभारत के सभी पात्रों पर कुछ-न-कुछ लांछन लगा हुआ है, पर कर्ण इस दृष्टि से सभी प्रकार से उज्ज्वल है। उसने जीवन में केवल एक बार झूठ बोला और वह भी धनुर्विद्या सीखने के लिए। किसी को धोखा देने अथवा हानि पहुँचाने वाले असत्य भाषण से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।
इन सबके अतिरिक्त कर्ण सच्चा मित्र, अद्वितीय दानी, निर्भीक, दृढ़प्रतिज्ञ तथा महान् योद्धा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर्ण उदात्त स्वभाव वाला धीर-वीर नायक है।
प्रश्न 8:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर कर्ण तथा दुर्योधन के चरित्र की तुलना कीजिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय ‘प्रेमी’ कृते ‘सूते-पुत्र’ नाटक में कर्ण मुख्य पात्र है और दुर्योधन गौण पात्र। दुर्योधन के चरित्र को समायोजन इस नाटक में कर्ण के चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट करने एवं ऐतिहासिक तत्त्वों को प्रासंगिक बनाने के लिए किया गया है।
कर्ण एवं दुर्योधन का चरित्र-चित्रण
(1) नारी के प्रति श्रद्धा भाव – कर्ण नारी जाति के प्रति निष्ठावान एवं श्रद्धावान है। यद्यपि वह अपनी माता की भूल के कारण आजीवन दुःख और अपमान सहता है, तथापि उसके मन में नारी के लिए असीम आदर की भावना विद्यमान है। वह कहता है-”नारी विधाता का वरदान है। “नारी सत्यता, संस्कृति की प्रेरणा है। नारी का अपहरण कभी भी सह्य नहीं हो सकता।” दुर्योधन की भावना नारी के प्रति कर्ण की भावना के बिल्कुल विपरीत है। उसके मन में नारी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तभी तो वह द्रौपदी का अपहरण कर लेना चाहता है।
(2) सच्चा तथा विश्वासपात्र मित्र – कर्ण एक सच्चा तथा विश्वास करने योग्य मित्र है। इसी कारण दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बनाता है। वह जीवन भर उसकी मित्रता का निर्वाह करता है। दूसरी ओर दुर्योधन भी एक सफल कूटनीतिज्ञ तथा मित्रता का निर्वाह करने वाला राजपुरुष है।
(3) प्रबल नैतिकता – कर्ण उच्चकोटि के संस्कारों से युक्त है, अत: वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्त्व प्रदान करता है। द्रौपदी के अपहरण कर लेने की बात पर कर्ण दुर्योधन से कहता है-“दूसरे अनुचित करते हैं इसलिए हम भी अनुचित करें, यह नीति नहीं है। किसी की पत्नी का अपहरणपरम्परा से निन्दनीय है।” दुर्योधन नीति सम्बन्धी तथ्यों को नहीं मानता और द्रौपदी का अपहरण कर लेना चाहता है। उसके चरित्र में यह एक बड़ा दोष है।
(4) विचारवान्सू – त-पुत्र’ नाटक का प्रमुख पात्र ‘कर्ण’ एक विचारवान् और सुन्दर युवक होने के
साथ-ही-साथ गुरुभक्त भी है। गुरु से शापित होने पर भी वह गुरु की अवज्ञा नहीं करता है। कर्ण में वीरोचित सभी गुण विद्यमान हैं। दुर्योधन वीर और महत्त्वाकांक्षी तो है, परन्तु विचारवान् नहीं है। कर्ण के रथ का सारथी शल्य को बनाते समय वह उसके स्वभाव के सम्बन्ध में नहीं सोचता है। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्ण और दुर्योधन परम मित्र होते हुए भी विरोधी भावनाओं और गुणों से युक्त हैं।
प्रश्न 9:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के आधार पर श्रीकृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
श्रीकृष्ण का चारित्र-चित्रण
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक का कथानक संस्कृत के महाकाव्य महाभारत’ पर आधारित है। यद्यपि इस नाटक का कंथानक पूर्ण रूप से कर्ण को केन्द्रबिन्दु मानकर ही अग्रसर होता है, परन्तु श्रीकृष्ण भी एक प्रभावशाली पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं।
प्रस्तुत नाटक में श्रीकृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं को निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है-
(1) वीरता के प्रशंसक – यद्यपि श्रीकृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और उसके सारथी भी, परन्तु वे कर्ण की वीरता एवं शक्ति के प्रशंसक हैं। उन्हें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि कर्ण सभी प्रकार से सुरक्षित अर्जुन के रथ को पीछे हटा देता है। वे कहते हैं – ”धन्य हो कर्ण ! तुम्हारे समान धनुर्धर सम्भवतः पृथ्वी पर दूसरा नहीं है।”
(2) कुशल राजनीतिज्ञ – कर्ण के पास, सूर्य के द्वारा दिये गये कवच-कुण्डलों को इन्द्र को दान कर देने पर, इन्द्र से प्राप्त एक अमोघ शक्ति थी जिसे कर्ण अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखना चाहता है; परन्तु श्रीकृष्ण कर्ण की उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कचे पर करा देते हैं। यह श्रीकृष्ण की दूरदर्शिता एवं कुशल राजनीति का ही परिणाम था।
(3) कुशल वक्ता – श्रीकृष्ण कुशल वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण नहीं चलाना चाहता था। श्रीकृष्ण उसके भावों को उत्तेजित करते हैं और इस तरह बात करते हैं कि अर्जुन को धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है।
(4) अवसर को न चूकने वाले – कर्ण के ऊपर बाण छोड़ने के लिए वे अर्जुन से कहते हैं – ”अगर तुम इस अवस्था में कर्ण पर बाण नहीं चलाओगे तो दूसरी अवस्था में वह तुम्हें बाण चलाने नहीं देगा।” वे अर्जुन से कहते हैं–”यही समय है, जब तुम कर्ण को अपने बाणों का लक्ष्य बनाकर सदा के लिए युद्ध-भूमि में सुला सकते हो।’ ………शीघ्रता करो ! अवसर का लाभ उठाओ।”
(5) महाज्ञानी – श्रीकृष्ण ज्ञानी पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। वे अर्जुन से कहते हैं-“मृत्यु को देखकर बड़े-बड़े योद्धा, तपस्वी और ज्ञानी तक व्याकुल हो उठते हैं।” वे अर्जुन को समझाते हैं “शरीर के साथ आत्मा को बन्धन बहुत दृढ़ होता है।” इस प्रकार उनके ज्ञान और विद्वत्ता का स्पष्ट आभास मिलती है।
(6) पश्चात्ताप की भावना – श्रीकृष्ण को इस बात का पश्चात्ताप है कि कर्ण का वध न्यायोचित ढंग से नहीं हुआ। वे मानते हैं-”हमने अपनी विजय-प्राप्ति के स्वार्थवश कर्ण के साथ जो कुछ अन्याय किया है, हम इस प्रकार यश दिलाकर उसे भी थोड़ा हल्का कर सकेंगे।”
अस्तु; श्रीकृष्ण रंगमंच पर यद्यपि कुछ देर के लिए नाटक के अन्त में ही आते हैं, तथापि इतने से ही उनके : व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से मिल जाती है।
प्रश्न 10:
‘सूत-पुत्र नाटक के आधार पर कुन्ती का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक के प्रमुख नारी-पात्र का चरित्र-चित्रण कीजिए।
उत्तर:
कुन्ती का चरित्र-चित्रण
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक की प्रमुख नारी-पात्र है कुन्ती। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
(1) मातृ-भावना – कुन्ती का हृदय मातृ-भावना से परिपूर्ण है। युद्ध का निश्चय सुनते ही वह अपने पुत्रों के कल्याण के लिए व्याकुल हो उठती है। यद्यपि उसने कर्ण का परित्याग कर दिया था और किसी के सामने भी उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था; किन्तु अपने मातृत्व के बल पर ही वह उसके पास जाती है। और कहती है-“तुम मेरी पहली सन्तान हो कर्ण ! मैंने लोकापवाद के भय से ही तुम्हारा त्याग किया था।”
(2) कुशल नीतिज्ञ – कुन्ती अपने पुत्रों की विजय और कुशल-क्षेम के लिए अपने त्यक्त-पुत्र कर्ण (जिसे असवर्ण घोषित कर दिया गया था) को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। जब कर्ण यह कहता है कि पाण्डव यदि मुझे सार्वजनिक रूप में अपना भाई स्वीकार करें तब ही उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो सकता है, तो कुन्ती तत्काल ही कह देती है—“कर्णं तुम्हारे पाँचों अनुज सार्वजनिक रूप से तुम्हें अपना अग्रज स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं।” जब कि पाण्डवों को उस समय तक यह भी नहीं मालूम हो पाया था कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं। कुन्ती उसे राज्य एवं द्रौपदी के पाने का भी लालच दिखाती है, जो स्वयंवर के समय उसे असवर्ण कहकर अस्वीकार कर चुकी थी। इस प्रकार उसमें राजनीतिक कुशलता भी पूर्ण रूप से विद्यमान थी।
(3) स्पष्टवादिता – स्पष्टवादिता कुन्ती के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। वह माता होकर भी अपने पुत्र कर्ण के सामने अपने कौमार्य में उसे जन्म देने के प्रसंग और उसे अपना पुत्र होने की बात कहते नहीं हिचकती। कर्ण द्वारा यह पूछे जाने पर कि तुमने किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूर्यदेव से सम्पर्क स्थापित किया, वह कहती है-“पुत्र! तुम्हारी माता के मन में वासना का भाव बिल्कुल नहीं था।” जब कर्ण उससे यह पूछता है कि विवाह के बाद तुमने देव-ओह्वान मन्त्र का क्यों उपयोग किया; तब कुन्ती अपने पति की शापजन्य असमर्थता का उल्लेख करती है और बताती है कि वे–पाण्डु तथा धृतराष्ट्र-भी “अपने पिताओं की सन्तान नहीं, मात्र माताओं की सन्तान हैं।”
(4) वाक्पटु – कुन्ती बातचीत में भी बहुत कुशल है। वह अपनी बातें इतनी कुशलता से कहती है कि कर्ण एक नारी, एक माँ की विवशता को समझकर उसकी भूलों पर ध्यान न दे तथा उसकी बात मान ले। वह कर्ण की बातों में निहित भावों को समझ जाती है और उनका तत्काल तर्कपूर्ण उत्तर देती है। वह कर्ण को पहले पुत्र और बाद में कर्ण कहकर अपने मनोभावों को प्रदर्शित कर देती है और इस प्रकार अपनी वाक्-पटुता का परिचय देती है। वह कहती है-“चलती हूँ पुत्र ! नहीं, नहीं, कर्ण ! मुझे तुम्हारे आगे याचना करके भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।”
(5) सूक्ष्म दृष्टि – कुन्ती में प्रत्येक विषय को परखने और तदनुकूल कार्य करने की सूक्ष्म दृष्टि थी। कर्ण जब उससे कहता है कि तुम यह कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ जिसको तुमने गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया था; तब कुन्ती उससे कहती है-”क्या तुम्हारे पैरों की अँगुलियाँ मेरे पैरों की अँगुलियों से मिलती-जुलती नहीं हैं।”
इस प्रकार नाटककार ने थोड़े ही विवरण में कुन्ती के चरित्र को कुशलता से दर्शाया है। नाटककार ने विभिन्न स्थलों पर कुन्ती के कथनों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक माता द्वारा पुत्रों के कल्याण की कामना करना उसका स्वार्थ नहीं, वरन् उसकी सहज प्रकृति का परिचायक है।
प्रश्न 11:
परशुराम का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
परशुराम का चरित्र-चित्रण
डॉ० गंगासहाय प्रेमी द्वारा रचित ‘सूत-पुत्र’ नाटक में परशुराम को ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व के गुणों से समन्वित महान् तेजस्वी और दुर्धर्ष योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। परशुराम कर्ण के गुरु हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि है। परशुराम अपने समय के धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता थे। नाटक के अनुसार इनकी चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन निम्नवत् है
(1) ओजयुक्त व्यक्तित्व – परशुराम का व्यक्तित्व ओजयुक्त है। नाटककार ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण इस प्रकार किया है-”परशुराम की अवस्था दो सौ वर्ष के लगभग है। वे हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले सुदृढ़ व्यक्ति हैं। चेहरे पर सफेद, लम्बी-घनी दाढ़ी और शीश पर लम्बी-लम्बी श्वेत जटाएँ हैं।”
(2) महान् धनुर्धर – परशुराम अद्वितीय धनुर्धारी हैं। सुदूर प्रदेशों से ब्राह्मण बालक इनके पास हिमालय की घाटी में स्थित आश्रम में शस्त्र-विद्या ग्रहण करने आते हैं। इनके द्वारा दीक्षित शिष्यों को उस समय अद्वितीय माना जाता था। भीष्म पितामह भी इन्हीं के प्रिय शिष्यों में से एक थे।
(3) मानव-स्वभाव के पारखी-परशुराम मानव – स्वभाव के अचूक पारखी हैं। वे कर्ण के क्षत्रियोचित व्यवहार से जाने जाते हैं कि यह ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय-पुत्र है। वे उससे निस्संकोच कहते हैं “तुम क्षत्रिय हो कर्ण! तुम्हारे माता-पिता दोनों ही क्षत्रिय रहे हैं।”
(4) आदर्श गुरु – परशुराम एक आदर्श गुरु हैं। वे शिष्यों को पुत्रवत् स्नेह करते हैं और उनके कष्ट-निवारण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कर्ण की जंघा में कीड़ा काट लेता है और मांस में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे परशुराम का हृदय द्रवित हो उठता है। वे तुरन्त उसके घाव पर नखरंजनी का प्रयोग करते हैं और कर्ण को सान्त्वना देते हैं। यह घटना गुरु परशुराम के सहृदय होने को प्रमाणित करती है।
(5) श्रेष्ठ ब्राह्मण – परशुराम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वे विद्या-दान को ब्राह्मण का सर्वप्रमुख कार्य मानते हैं। जो ब्राह्मण धनलोलुप हैं, परशुराम की दृष्टि में वे नीच तथा पतित हैं, इसीलिए वे द्रोणाचार्य को निम्नकोटि का ब्राह्मण मानते हैं और कहते हैं-”द्रोणाचार्य तो पतित ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का गुरु हो सकता है, सेवक अथवा वृत्तिभोगी नहीं।”
(6) उदारमना – परशुराम सहृदय तथा उदारमना हैं। वे अपने कर्तव्यपालन में वज्र के समान कठोर हैं, लेकिन दूसरों की दयनीय दशा को देखकर द्रवीभूत भी हो जाते हैं। ब्राह्मण का छद्म रूप धारण करने के कारण वे कर्ण को शाप दे देते हैं, लेकिन जब कर्ण की शोचनीय तथा दुःख-भरी दशा का अवलोकन करते हैं तो वे उसके प्रति सहृदय हो जाते हैं। वे कहते हैं-”जिस माता से तुम्हें ममता और वात्सल्य मिलना चाहिए था, उससे तुमने कठोर निर्मम निर्वासन पाया। जिस गुरु से तुम्हें वरदान मिलना चाहिए था, उसी ने तुम्हें शाप दिया।” उनके इस कथन से उनके उदारमना होने की पुष्टि होती है।
(7) कर्तव्यनिष्ठ – परशुराम एक कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। कर्त्तव्यपालन में वे बड़ी-से-बड़ी बाधाओं को सहर्ष स्वीकार करने को उद्यत रहते हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर कर्ण उनसे कहता है-”आपके हृदय में कोई कठोरता अथवा निर्ममता नहीं रही है। आपने जिसे कर्त्तव्य समझा है, जीवन भर उसी का पालन निष्ठापूर्वक किया है।”
(8) महाक्रोधी – यद्यपि परशुराम जी में अनेक गुण हैं, तथापि क्रोध पर अभी उन्होंने पूर्णतया विजय नहीं पायी है। क्रोध में आकर वे अपने महान् त्यागी शिष्य कर्ण को भी जब शाप दे देते हैं तो संवेदनशील पाठक का हृदय हाहाकार कर उठता है। वह मानव मन के इस विकराल विकार को, ऋषियों तक को अपना शिकार बनाते देखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परशुराम तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण हैं। वे एक आदर्श शिक्षक तथा उदार हृदय के स्वामी हैं। उनमें ब्राह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व दोनों के गुणों का अद्भुत समन्वय है।
प्रश्न 12:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के नायक कर्ण के अन्तर्द्वन्द्व पर प्रकाश डालिए।
या
“क्या सारा महत्त्व जाति का ही है ?” कर्ण के इस संवाद के माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका वर्णन कीजिए।
या
“कर्ण आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है।’ विश्लेषित कीजिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक के नायक कर्ण का मानसिक अन्तर्द्वन्द्व कई स्थानों पर । उसके संवादों के माध्यम से प्रकट होता है। प्रथम चरण में वह अपने गुरु परशुराम के सामने इस द्वन्द्व को प्रकट करता है। वह जानना चाहता है कि क्या उसकी अयोग्यता मात्र इसलिए है कि वह किसी विशेष जाति से सम्बन्धित है। दूसरी बार द्रौपदी स्वयंवर में वह द्रुपद-नरेश से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है। वह उनसे पूछता है। कि जब स्वयंवर में योग्यता का निर्धारण धनुर्विद्या की कसौटी पर किया जाना है तो कुल-शील, जाति अथवा वर्ण सम्बन्धी प्रतिबन्धों का क्या औचित्य है? उसका यही अन्तर्द्वन्द्व इन्द्र, सूर्य एवं कुन्ती के समक्ष भी प्रकट होता है। वह सामाजिक मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं की विसंगतियों के उत्तर चाहता है। वह प्रत्येक को अपनी विचारात्मक तर्कशक्ति के आधार पर इन विसंगतियों के प्रति सहमत कर लेता है, किन्तु उसे क्षोभ इस बात का है कि सभी अपनी विवशता प्रकट करते हुए इस लक्ष्मण-रेखा का अतिक्रमण करने से डरते हैं। कर्ण की व्यथा प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति के अन्तर्मन को गहराई से झकझोर देती है। नाटककार ने कर्ण के अन्तर्मन में उत्पन्न इन प्रश्नों के माध्यम से वर्तमान समय के जाति-वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी रूढ़ियों से ग्रस्त भारतीय समाज के विचारों पर चोट की है। कर्ण के प्रति हुए अन्याय की मूल समस्या अनेक महापुरुषों द्वारा प्रयास किये जाने के बाद भी हमारे देश में आज तक समाधान नहीं पा सकी है।
प्रश्न 13:
सूत-पुत्र’ के सर्वाधिक मार्मिक स्थल पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत ‘सूत-पुत्र’ नाटक में कर्ण की जीवन-लीला का अन्त; इस नाटक का सर्वाधिक मार्मिक स्थल है। कर्ण युद्धभूमि में आहत होकर मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। शरीर के छिन्न-भिन्न होने से वह अत्यन्त पीड़ा का अनुभव कर रहा है। इसी समय कृष्ण उसकी दानवीरता एवं साहस की परीक्षा लेने पहुँच जाते हैं। वे उससे ब्राह्मण-वेश में जाकर सुवर्ण का दान माँगते हैं। युद्ध-भूमि में कर्ण के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह उनसे अपने दो सोने के दाँत उखाड़ लेने का निवेदन करता है। कृष्ण के ऐसा करने से मना कर देने पर वह उनसे पत्थर देने का आग्रह करता है, जिससे वह अपने दाँत तोड़कर उन्हें दान दे सके। कृष्ण जब इससे भी मना कर देते हैं, तब वह घायलावस्था में घिसटते हुए पत्थर उठाता है और अपने दाँत तोड़कर उन्हें देता है। कृष्ण उन रक्तरंजित दाँतों को अपवित्र बताकर दान लेने से मना कर देते हैं। इस पर वह बड़ी कठिनाई से अपना धनुष उठाता है और धरती पर बाण का प्रहार करके जल की धारा प्रवाहित करता है तथा उस जलधारा में अपने टूटे हुए दाँत धोकर कृष्ण को देता है। प्रसन्न होकर कृष्ण उसके सामने अपने रूप को प्रकट करके उसे साधुवाद देते हैं।
नाटककार ने कर्ण के अन्तिम समय में कृष्ण द्वारा ली गयी इस परीक्षा का चित्रण करके कर्ण के चरित्र को महान् दानी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण ने स्वयं अपनी परीक्षा का उद्देश्य भी यही बताया है।
प्रश्न 14:
सूत-पुत्र’ नाटक के सन्देश पर प्रकाश डालिए।
या
‘सूत-पुत्र नाटक के उद्देश्य (प्रतिपाद्य) पर विचार व्यक्त कीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की रचना में नाटककार का क्या उद्देश्य था और उसकी पूर्ति में उसको कहाँ तक सफलता मिली है ? संक्षेप में लिखिए।
या
‘सूत-पुत्र में प्राचीन कथा में वर्तमान की समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
उत्तर:
‘सूत-पुत्र’ नाटक का सन्देश या उद्देश्य
लेखक श्री गंगासहाय प्रेमी की दृष्टि में ‘सूत-पुत्र’ नाटक का मुख्य उद्देश्य ‘महाभारत के मनस्वी, संघर्षशील एवं कर्मठ व्यक्तित्व कर्ण के प्रति पाठकों एवं दर्शकों की सहानुभूति उत्पन्न करता है। कुन्ती की एक सामान्य-सी भूल के परिणामस्वरूप कर्ण का सारा जीवन कष्टप्रद एवं अपमानजनक बन जाता है। इसी का उल्लेख प्रस्तुत नाटक में किया गया है।
इस मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त नाटककार ने अपने पात्रों के मुख से स्थान-स्थान पर नारी की विवशता, वर्ण-व्यवस्था की वास्तविकता, कुमारी माता की समस्या, असवर्गों के प्रति भेदभाव, नारी-शिक्षा, नैतिकता आदि के औचित्य के प्रति भी संकेत कराये हैं। नाटककार ने अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। नारी-शिक्षा के उद्देश्य को नाटककार ने कर्ण के मुख से इस प्रकार वर्णित कराया है
“पुरुषों ने यह कभी नहीं सोचा कि यदि नारियाँ शिक्षित, सन्तुष्ट, स्वस्थ एवं मनस्विनी नहीं होतीं तो उनके जन्मे एवं उनकी छाया में पले हुए पुरुषों में ये गुण कहाँ से आ सकते थे?”
महाभारत काल में समाज ने जिन समस्याओं का सामना किया था, लगभग वही सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएँ आधुनिक समाज में भी व्याप्त हैं। नाटककार ने वर्तमान काल की इन्हीं समस्याओं को महाभारत काल की कथा के माध्यम से स्वर दिया है।
प्रश्न 15:
डॉ० गंगासहाय प्रेमी ने अपने नाटक ‘सूत-पुत्र’ में प्राचीन कथा को आधार बनाकर वर्तमान की किन ज्वलन्त समस्याओं को चित्रित किया है ? संक्षिप्त उत्तर दीजिए।
या
‘सूत-पुत्र’ नाटक की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
‘सूत-पुत्र’ नाटक के लेखक डॉ० गंगासहाय प्रेमी ने सूत-पुत्र की कथा ‘महाभारत’ महाकाव्य से ली है। कथानक प्राचीन होते हुए भी वर्तमान काल की ज्वलन्त समस्याओं को सँजोये हुए है। जिन समस्याओं का निदान एवं समाधान खोजने में देश के नेता एवं समाज-सुधारक चिन्तित दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं समस्याओं का शिकार महाभारतकालीन समाज भी था। तत्कालीन समस्याओं का उल्लेख निम्नवत् किया जा सकता है
- अवैध सन्तान एवं जन-अपवाद की समस्या,
- वर्ण-भेद की जटिलता,
- क्षत्रिय एवं शूद्रों में व्याप्त भेदभाव,
- नारी के प्रति हीन भावना,
- नारी-अपहरण की समस्या,
- स्वार्थपरता,
- स्वार्थ-साधना के लिए छल-प्रपंच का प्रयोग तथा
- पारस्परिक ईष्र्या-द्वेष की भावना।
प्रश्न 16:
‘सूत-पुत्र नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
लेखक डॉ० गंगासहाय प्रेमी कृत सूतपुत्र एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग हुआ है। नाटक के पात्र और उसकी घटनाएँ महाभारत से सम्बन्धित हैं। नाटक के पात्र कर्ण, कुन्ती, परशुराम, दुर्योधन, श्रीकृष्ण आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कर्ण द्वारा झूठ बोलकर विद्या सीखना, पता चलने पर परशुराम का कर्ण को शाप देना; द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन का मछली की आँख को बेधना कर्ण द्वारा अपने परिचय से द्रुपद को सन्तुष्ट न कर पाना, द्रौपदी के लिए दुर्योधन का अर्जुन से संघर्ष करना, इन्द्र द्वारा कर्ण से कवच कुण्डल माँगना, कुन्ती का कर्ण को अपना ज्येष्ठ पुत्र बताना आदि प्रमुख महाभारतकालीन ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इस नाटक में ऐतिहासिक तत्त्वों को भी सफलतापूर्वक दर्शाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ‘सूत-पुत्र’ नाटक एक सफल ऐतिहासिक नाटक है।
प्रश्न 17:
सूत-पुत्र नाटक के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
उत्तर:
सम्पूर्ण नाटक की कथा ‘सूत-पुत्र कर्ण के इर्द-गिर्द ही घूमती है और कर्ण अपनी माता कुन्ती, इन्द्र और श्रीकृष्ण के समझाने पर भी सूत-पुत्र की छवि को त्यागकर क्षत्रिय राजकुमार कर्ण नहीं बनना चाहता। वह अपने आप को सूत-पुत्र बनाये रखकर दुर्योधन की मित्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देना चाहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक का ‘सूत-पुत्र’ शीर्षक सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi नाटक Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi नाटक Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.