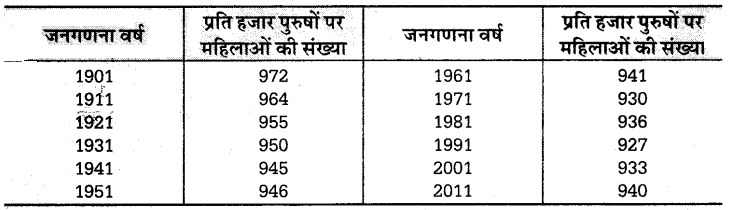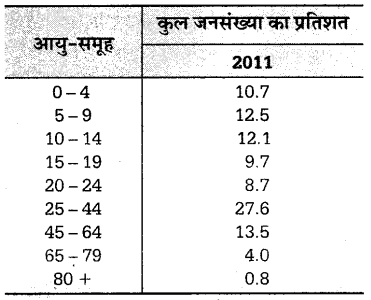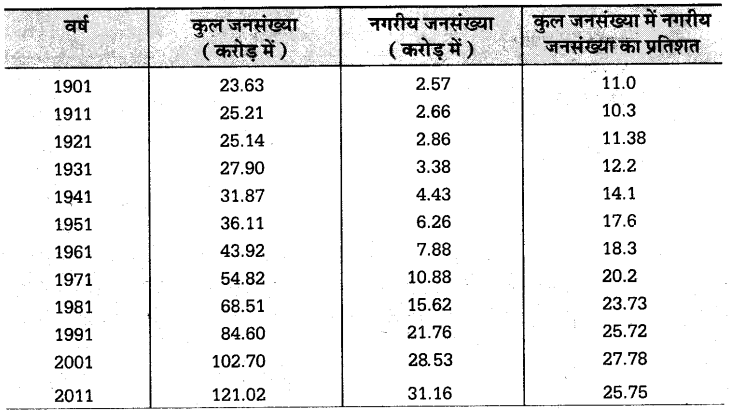UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण) are part of UP Board Solutions for Class 12 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Sociology |
| Chapter | Chapter 2 |
| Chapter Name | Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण) |
| Number of Questions Solved | 36 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1
प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण के समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए। [2007, 08, 10]
या
पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबन्ध लिखिए। [2010]
या
प्रदूषण के उत्तर दायी कारकों की विवेचना कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? आधुनिक भारत में प्रदूषण की समस्या का कारण क्या है? [2016]
या
पर्यावरण प्रदूषण के कौन-कौन से प्रमुख कारण हैं? [2009, 10, 14, 16]
या
पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसे समाप्त करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। प्रदूषण के स्रोतों की विवेचना कीजिए। [2015]
या
प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के कुप्रभावों का वर्णन कीजिए। [2010, 11]
या
पर्यावरण को जल-प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? [2017]
या
प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को समझाते हुए इनके नियन्त्रण के उपायों को समझाइए। [2015]
या
मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन कीजिए। [2016]
उत्तर :
पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं प्रकार
पर्यावरण प्रदषण का सामान्य अर्थ है – हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति-प्रदत्त पर्यावरण में जब किन्हीं तत्त्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसको जीवन के किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के स्थान पर अन्य विषैली एवं अनुपयोगी गैसों का अनुपात बढ़ जाए तो कहा। जाएगा कि वायु प्रदूषण हो गया है। वायु के अतिरिक्त पर्यावरण के किसी भी भाग के दूषित हो जाने को पर्यावरण प्रदूषण ही कहा जाएगा।
पर्यावरण के मुख्य भागों या पक्षों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों या स्वरूपों का निर्धारण किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं-जल-प्रदूषण, वायुप्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण तथा मृदा-प्रदूषण।
1. जल-प्रदूषण
जल में जीव रासायनिक ऑक्सीजन तथा विषैले रसायन, खनिज, ताँबा, सीसा, अरगजी, बेरियम फॉस्फेट, सायनाइड आदि की मात्रा में वृद्धि होना ही जल-प्रदूषण है। जल-प्रदूषण दो प्रकार का होता है
- दृश्य – प्रदूषण तथा
- अदृश्य – प्रदूषण।
जल-प्रदूषण के कारण – जल-प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है–
- औद्योगीकरण जल-प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तर दायी है। चमड़े के कारखाने, चीनी एवं ऐल्कोहॉल के कारखाने, कागज की मिलें तथा अन्य अनेकानेक उद्योग नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं।
- नगरीकरण भी जल-प्रदूषण के लिए उत्तर दायी है। नगरों की गन्दगी, मल व औद्योगिक अपशिष्टों के विषैले तत्त्व भी जल को प्रदूषित करते हैं।
- समुद्रों में जहाजरानी एवं परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से भी जल प्रदूषित होता है।
- नदियों के प्रति भक्ति-भाव होते हुए भी तमाम गन्दगी; जैसे-अधजले शव, जानवरों की लाशें तथा अस्थि-विसर्जन आदि-भी नदियों में ही किया जाता है, जो नदियों के जल प्रदूषण का एक कारण है।
- जल में अनेक रोगों के हानिकारक कीटाणु मिल जाते हैं, जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो जाता
- भूमिक्षरण के कारण मिट्टी के साथ रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक पदार्थों के नदियों में पहुँच जाने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है।
- घरों से बहकर निकलने वाला फिनायल, साबुन, सर्फ आदि से युक्त गन्दा पानी तथा शौचालय का दूषित मल नालियों में प्रवाहित होता हुआ नदियों और झील के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है।
- नदियों और झीलों के जल में पशुओं को नहलाना, पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा स्नान करना वे साबुन आदि से गन्दे वस्त्र धोना भी जल-प्रदूषण का मुख्य कारण है।
जल-प्रदूषण रोकने के उपाय – जल की शुद्धता और उपयोगिता बनाये रखने के लिए प्रदूषण को रोकना आवश्यक है। जल-प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये जा सकते हैं
- नगरों के दूषित जल और मल को नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में मिलने से रोका जाए।
- कल-कारखानों के दूषित और विषैले जल को नदियों और झीलों के जल में न गिरने दिया जाए।
- मल-मूत्र एवं गन्दगीयुक्त जल का उपयोग बायोगैस बनाने या सिंचाई के लिए करके प्रदूषण को रोका जा सकता है।
- सागरों के जल में आणविक परीक्षण न कराए जाएँ।
- नदियों के तटों पर शव ठीक से जलाए जाएँ तथा उनकी राख भूमि में दबा दी जाए।
- पशुओं के मृतक शरीर तथा मानव शवों को स्वच्छ जल में प्रवाहित न करने दिया जाए।
- जल-प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाये जाएँ तथा उनका कठोरता से पालन किया जाए।
- नदियों, कुओं, तालाबों और झीलों के जल को शुद्ध बनाये रखने के लिए प्रभावी उपाय काम में लाये जाएँ।
- जल-प्रदूषण के कुप्रभाव तथा रोकने के उपायों का जनसामान्य में प्रचार-प्रसार कराया जाए।
- जल उपयोग तथा जल-संसाधन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनायी जाए।
जल-प्रदूषण का मानव-जीवन पर प्रभाव (हानियाँ) – जब से सृष्टि है-पानी है; यह सर्वाधिक बुनियादी और महत्त्वपूर्ण साधन है। ‘पानी नहीं तो जीवन नहीं।’ संसार का 4 प्रतिशत पानी पृथ्वी पर है, शेष पानी समुद्रों में है, जो खारा है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका केवल 0.3 प्रतिशत भाग ही साफ और शुद्ध है और इसी पर सारी दुनिया निर्भर है। आज शुद्ध पानी कम होता जा रहा है और प्रदूषित पानी दिन-प्रतिदिन अधिक। प्रदूषित जल मानव-जीवन को निम्नलिखित प्रकार से सर्वाधिक प्रभावित करता है
- जल, जो जीवन की रक्षा करता है, प्रदूषित हो जाने पर जीव की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता है और बनता जा रहा है।
- जल-प्रदूषण से अनेक बीमारियाँ; जैसे-हैजा, पीलिया, पेट में कीड़े, यहाँ तक कि टायफाइड भी प्रदूषित जल के कारण ही होता है, जिससे विकासशील देशों में पाँच में से चार बच्चे पानी की गन्दगी के कारण उत्पन्न रोगों से मरते हैं।
राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी गाँवों में गन्दे तालाबों का पानी पीने से “नारू’ नाम का भयंकर रोग होता है। इन गाँवों के 6 लाख 90 हजार लोगों में से 1 लाख 90 हजार लोगों को यह रोग है। - प्रदूषित जल का प्रभाव जल में रहने वाले जन्तुओं और जलीय पौधों पर भी पड़ रहा है। जल-प्रदूषण के कारण मछली और जलीय पौधों में 30 से 50 प्रतिशत तक की कमी हो गयी है। जो व्यक्ति खाद्य-पदार्थ के रूप में मछली आदि का उपयोग करते हैं, उनके स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है।।
- प्रदूषित जल का प्रभाव कृषि-उपजों पर भी पड़ता है। कृषि से उत्पन्न खाद्य-पदार्थों को मानव व पशुओं के उपयोग में लाते हैं, जिससे मानव व पशुओं के स्वास्थ्य को हानि होती
- जल-जन्तुओं के विनाश से पर्यावरण असन्तुलित होकर विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव उत्पन्न करता है।
2. वायु-प्रदूषण
वायु में विजातीय तत्त्वों की उपस्थिति चाहे गैसीय हो या पार्थक्य या दोनों का मिश्रण, जो कि मानव के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो, वायु-प्रदूषण कहलाता है।
वायु-प्रदूषण मुख्य रूप से धूलकण, धुआँ, कार्बन-कण, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, कैडमियम आदि घातक पदार्थों के वायु में मिलने से होता है। ये सब उद्योगों एवं परिवहन के साधनों के माध्यम से वायुमण्डल में मिलते हैं।
वायु-प्रदूषण के कारण – वायु-प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है
- नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं अनियन्त्रित भवन-निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है।
- परिवहन के साधनों (ऑटोमोबाइलों) से निकलता धुआँ वायु-प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण
- नगरीकरण एवं नगरों की बढ़ती गन्दगी भी वायु को प्रदूषित कर रही है।
- वनों की अनियमित एवं अनियन्त्रित केटाई से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
- रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक औषधियों के कृषि में अधिकाधिक उपयोग से भी वायु-प्रदूषण बढ़ रहा है।
- रसोईघरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएँ के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
- विभिन्न प्रदूषकों के भूमि पर फेंकने से वायु-प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है।
- दूषित जल-मल के एकत्र होकर दुर्गन्ध फैलाने से वायु प्रदूषित हो रही है।
- युद्ध, आणविक विस्फोट तथा दहन की क्रियाएँ वायु-प्रदूषण उत्पन्न करती हैं।
- कीटनाशक पदार्थों के छिड़काव के कारण वायुमण्डल प्रदूषित हो जाता है।
वायु-प्रदूषण रोकने के उपाय – वायु मानव-जीवन का मुख्य आधार है। वायु का प्रदूषण मानव-जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी उपाय ढूंढ़ना आवश्यक है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये जा सकते
- कल-कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करना तथा उनसे निकलने वाले धुएँ, गैस तथा राख पर नियन्त्रण करना।
- परिवहन के साधनों पर धुआं-रहित यन्त्र लगाना।
- नगरों में हरित पट्टी के रूप में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कराना।
- नगरों में स्वच्छता, जल-मल निकास तथा अवशिष्ट पदार्थों के मार्जन की उचित व्यवस्था करना।
- वन लगाने तथा वृक्ष संरक्षण पर बल देना।
- रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को नियन्त्रित करना।
- घरों में बायोगैस, पेट्रोलियम गैस या धुआँ-रहित चूल्हों का प्रयोग करना।
- खुले में मैला, कूड़ा-करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए न फेंकना।
- गन्दा जल एकत्र न होने देना।
- वायु-प्रदूषण रोकने के लिए कठोर नियम बनाना और दृढ़ता से उनका पालन कराना।
वायु-प्रदूषण का मानव-जीवन पर प्रभाव – वायु-प्रदूषण के मानव-जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं
- वायु-प्रदूषण से जानलेवा बीमारियाँ; जैसे-छाती और साँस की बीमारियाँ, ब्रांकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर आदि बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
- वायु-प्रदूषण मानव-शरीर, मानव की खुशियों और मानव की सभ्यता के लिए खतरा बना हुआ है। नीला, भूरा, सफेद, तरह-तरह का परिवहन के साधनों का धुआँ पूँघता हुआ आदमी जब सड़कों पर चलता है तो वह नहीं जानता कि यह धुआँ उसकी आँखों में ही डंक नहीं मार रहा है, उसके गले को भी दबाता है और उसके फेफड़ों को भी जहरीले नाखूनों से नोच रहा है।
- वायु प्रदूषण न केवल चारों ओर फैले खेतों, हरे-भरे पेड़ों, रमणीक दृश्यों को भी धुंधला करता है व उन पर झीनी चादर डालता है, बल्कि खेतों, तालाबों व जलाशयों को अपने – कृमिकणों से विषाक्त करता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- डॉक्टरों ने परीक्षण कर देखा है कि जहाँ वायु-प्रदूषण अधिक है वहाँ बच्चों की हड्डियों का विकास कम होता है, हड्डियों की उम्र घट जाती है तथा बच्चों में खाँसी और सॉस फूलना तो देखा ही जा सकता है।
- वायु-प्रदूषण का प्रभाव वृक्षों पर भी देखा जा सकता है। चण्डीगढ़ के पेड़ों और लखनऊ के दशहरी आमों पर वायु-प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को देखा गया है, जिससे मानव को फल तो कम मात्रा में मिल ही रहे हैं, किन्तु जो मिल रहे हैं वे भी विषाक्त हैं, जिसको सीधा प्रभाव मानव पर पड़ रहा है।
- दिल्ली के वायुमण्डल में व्याप्त प्रदूषण का प्रभाव आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर तो पड़ा ही, दिल्ली की परिवहन पुलिस पर भी पड़ा है और यही दशा कोलकाता और मुम्बई की | भी है, अर्थात् इससे मानव का जीवन (आयु) घट रहा है।
- वायु-प्रदूषण के कारण ही फेफड़ों का कैंसर, टी० बी० तथा अन्य घातक रोग फैल रहे हैं।
- वायु-प्रदूषण के कारण ओजोन की परत में छेद होने की सम्भावना व्यक्त होने से सम्पूर्ण विश्व भयाक्रान्त हो उठा है।
- शुद्ध वायु न मिलने से शारीरिक विकास रुक गया है तथा शारीरिक क्षमता घटती जा रही है।
- वायु-प्रदूषण मानव अस्तित्व के सम्मुख एक गम्भीर समस्या बन कर खड़ा हो गया है, जिसे रोकने में भारी व्यय करना पड़ रहा है।
3. ध्वनिप्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप ध्वनि-प्रदूषण भी है। ध्वनि-प्रदूषण की समस्या नगरों में अधिक है। ध्वनि-प्रदूषण को साधारण शब्दों में शोर बढ़ने के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पर्यावरण में शोर अर्थात् ध्वनियों का बढ़ जाना ही ध्वनि-प्रदूषण है। अब प्रश्न उठता है कि शोर क्या है? वास्तव में, प्रत्येक अनचाही तथा तीव्र आवाज शोर है। शोर का बढ़ना ही ध्वनि-प्रदूषण का बढ़ना कहा जाता है।
ध्वनि-प्रदूषण के कारण – ध्वनि-प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तर दायी हैं
- ध्वनि-प्रदूषण परिवहन के साधनों; जैसे—बसों, ट्रकों, रेलों, वायुयानों, स्कूटरों आदि के द्वारा होता है। धड़धड़ाते हुए वाहन कर्कश स्वर देकर शोर उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है।
- कारखानों की विशालकाय मशीनें, कल-पुर्जे, इंजन आदि भयंकर शोर उत्पन्न करके ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बने हुए हैं।
- मस्जिदों में ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों से होने वाली अजान, मन्दिरों में भजन, कीर्तन तथा गुरुद्वारों में शबद कीर्तन भी प्रदूषण के कारण हैं।
- विभिन्न प्रकार के विस्फोटक भी ध्वनि-प्रदूषण के जन्मदाता हैं।
- घरों पर जोर से बजने वाले रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकॉर्डर, कैसेट्स तथा बच्चों की चिल्ल-पौं की ध्वनि भी प्रदूषण उत्पन्न करने के मुख्य साधन हैं।
- वायुयान, सुपरसोनिक विमान व अन्तरिक्ष यान भी ध्वनि-प्रदूषण फैलाते हैं।
- मानव एवं पशु-पक्षियों द्वारा उत्पन्न शोर भी ध्वनि-प्रदूषण का मुख्य कारण है।
- आँधी, तूफान तथा ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप भी ध्वनि-प्रदूषण उत्पन्न होता
ध्वनि-प्रदूषण रोकने के उपाय-डॉ० पी० सी० शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं
- ध्वनि-प्रदूषण निरोधक कानूनों को बनाना तथा उन्हें अमल में लाना।।
- कम शोर करने वाली मशीनों को बनाना।
- इमारतों के बाहर पेड़-पौधों, घास-झाड़ियों तथा घरों के अन्दर ध्वनि-शोषक साज-सज्जा एवं भवन निर्माण सामग्री का उपयोग करके ध्वनि-प्रदूषण के प्रभाव को कम करना।
- सामाजिक दबाव बनाकर ध्वनि-प्रदूषण फैलाने वाले यन्त्रों को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों को आवासीय बस्तियों तथा मनोरंजन के स्थानों से पृथक् करना।
- जिन उद्योगों में तीव्र ध्वनि को नियन्त्रित करना सम्भव नहीं है, वहाँ कामगारों को श्रवणेन्द्रियों की रक्षा हेतु कान में लगायी जाने वाली उपयुक्त रक्षा-डाटों को उपलब्ध कराना।
- जनसाधारण को ध्वनि-प्रदूषण के कुप्रभावों के प्रति जन-जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से सचेत करना तथा संवेदनशील बनाना।।
- स्कूलों में ध्वनि-प्रदूषण के विषय में ज्ञान देना।
ध्वनि-प्रदूषण का मानव-जीवन पर प्रभाव – ध्वनि-प्रदूषण का मानव-जीवन पर निम्नलिखित कुप्रभाव पड़ता है–
- ध्वनि-प्रदूषण मानव के कानों के परदों पर, मस्तिष्क और शरीर पर इतना घातक आक्रमण करता है कि संसार के सारे वैज्ञानिक तथा डॉक्टर इससे चिन्तित हो रहे हैं।
- ध्वनि-प्रदूषण वायुमण्डल में अनेक समस्याएँ उत्पन्न करता है और मानव के लिए एक गम्भीर खतरा बन गया है। जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोक ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब आदमी को अपने स्वास्थ्य के इस सबसे नृशंस शत्रु ‘शोर’ से पूरे जी-जान से लड़ना पड़ेगा।
- ध्वनि-प्रदूषण के कारण व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है तथा स्वास्थ्य खराब होने लगता है।
- शोर के कारण सुनने की शक्ति कम होती है। बढ़ते हुए शोर के कारण मानव समुदाय बहरेपन की ओर बढ़ रहा है।
- ध्वनि-प्रदूषण के कारण मानसिक तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है।
- ध्वनि-प्रदूषण मनुष्य के आराम में बाधक बनता जा रहा है।
ध्वनि-प्रदूषण की समस्या दिन-प्रति – दिन बढ़ती जा रही है। इस अदृश्य समस्या का निश्चित समाधान खोजना नितान्त आवश्यक है। विक्टर गुएन ने ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “शोर मृत्यु का मन्द गति अभिकर्ता है। यह मानव-मात्र का एक अदृश्य शत्रु है।”
वास्तव में, जल, वायु और ध्वनि-प्रदूषण आज के सामाजिक जीवन की एक गम्भीर चुनौती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरा है। बढ़ते प्रदूषण ने मानव सभ्यता, संस्कृति तथा अस्तित्व पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। भावी पीढ़ी को इस विष-वृक्ष से बचाये रखने के लिए प्रदूषण का निश्चित समाधान खोजना आवश्यक है।
4. मृदा-प्रदूषण
भूमि पेड़-पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक लवण, खनिज तत्त्व, जल, वायु तथा कार्बनिक पदार्थ संचित रखती है। भूमि में उपर्युक्त पदार्थ प्रायः निश्चित अनुपात में पाये जाते हैं। इन पदार्थों की मात्रा में किन्हीं प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा-प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, “भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है। अथवा जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, मृदा-प्रदूषण कहलाता है।”
मृदा-प्रदूषण के कारण मृदा-प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
- नगरों द्वारा ठोस कूड़ा-करकट फेंकने से तथा खानों के पास बेकार पदार्थों के ढेर जमा होने से भूमि अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती।
- दूषित क्षेत्रों से बहकर आया जल नदियों को प्रदूषित करता है। इन्हीं क्षेत्रों से जल का रिसाव भूमिगत जल में प्रदूषण फैलाता है।
- सिंचाई से भी भूमि का प्रदूषण होने लगा है। सिंचित भूमि पर नमक या नमकीन परत जम जाती है, ऐसी भूमि खेती योग्य नहीं रहती।
- अर्द्धमरुस्थलीय प्रदेशों में पवनें भारी मात्रा में बालू उड़ाकर पास-पड़ोस के खेतों में जमा कर देती हैं और खेत कृषि के लिए बेकार हो जाते हैं।
- बाढ़ के दौरान कंकड़, पत्थर तथा रेत जमा हो जाने से खेत बर्बाद हो जाते हैं।
- प्रदूषित जल तथा वायु के कारण मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। वर्षा इत्यादि के जल के साथ ये प्रदूषक पदार्थ मिट्टी में आ जाते हैं; जैसे-वायु में SO, वर्षा के जल के साथ मिलकर H,SO, अम्ल बना लेती है।
- इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ अधिक फसल पैदा करने के लिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने या बनाये रखने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक पदार्थ (Pesticides), अपतृणनाशी पदार्थ (weedicides) आदि फसलों पर छिड़के जाते हैं। ये सभी पदार्थ मृदा के साथ मिलकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
मृदा-प्रदूषण रोकने के उपाय – जैव-पदार्थ पौधे तथा मृदा के लिए उपयोगी हैं। खेती करने, वर्षा, भूमि का कटाव तथा कुछ अन्य कारणों से भूमि में जैव-पदार्थों की कमी होने लगती है। मृदा-प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए
- मृदा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए।
- खेत में सदैव कम सिंचाई करनी चाहिए।
- खेत में जल-निकास का उचित प्रबन्ध होना चाहिए।
- खेतों की मेड़बन्दी करनी चाहिए, जिससे वर्षा के पानी से या भूमि के कटाव से जीवांश पदार्थ बहकर न निकल जाएँ।
- विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, साबुन व अपमार्जक, अपतृणनाशक व अन्य रासायनिक पदार्थ आदि सामान्य मृदा प्रदूषक होते हैं। अतः इन पदार्थों से भूमि को बचाना चाहिए।
मृदा-प्रदूषण का मानव-जीवन पर प्रभाव – मृदा-प्रदूषण से मानव-जीवन पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं
- दूषित-मृदा में रोगों के जीवाणु पनपते हैं, जिनसे मनुष्यों व अन्य जीवों में रोग फैलते हैं।
- मृदा-प्रदूषण से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है।
- फसल की बर्बादी से जीव-जन्तुओं तथा मनुष्यों को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
यह स्पष्ट है कि अभी बताये गये उपायों को लागू करना केवल एक व्यक्ति के द्वारा सम्भव नहीं है। इस कार्य के लिए सरकार, विधिवेत्ताओं, वास्तुकारों, ध्वनि-अभियन्ता, नगर-परियोजना-अधिकारियों, पुलिस, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी।
प्रश्न 2
पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रथम कारण मानव सभ्यता का विकास ही है।’ स्पष्ट कीजिए। [2007, 12]
या
‘पारिस्थितिक-तन्त्र का पतन एवं पर्यावरण प्रदूषण’ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2011]
या
पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को व्यक्त कीजिए। [2012, 14, 16]
या
वायु-प्रदूषण में मानव-जनित प्रदूषण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रदूषण के दो कारकों का उल्लेख कीजिए। [2017]
उत्तर :
जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे-वैसे मानव की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जंगल काटकर खेती करना प्रारम्भ किया। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अब इस खेती को नष्ट करके मनुष्य उस पर मकान बनाने लगा है और फैक्ट्रियों में कार्य करके आज अपनी आजीविका कमा रहा है। विकास की तेज गति से मनुष्य को जहाँ लाभ पहुंचे हैं, वहाँ दूसरी ओर कई नुकसान भी हुए हैं। प्रकृति का सन्तुलन डगमगाने लगा है, उसकी सादगी और पवित्रता नष्ट हो रही है। अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मकान बनाने, खेती करने, ईंधन प्राप्त करने, पैसा बनाने तथा अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों और जंगलों का सफाया आज भी लगातार हो रहा है। प्रतिदिन नयी-नयी सड़कें, गगनचुम्बी इमारते, मिल, कारखाने आदि बन रहे हैं और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक साधनों का बहुत अधिक दोहन हो रहा है, हानिकारक रसायनों, गैसों व अन्य चीजों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इससे पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है और प्रदूषण पनप रहा है। हजारों वर्षों से मानव-जीवन पर्यावरण के सन्तुलन के सहारे चलता रहा है। मानव ने अपनी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हेतु पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया है कि इससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण का सर्वप्रमुख कारण मानव सभ्यता का विकास ही है
1. दहन – लकड़ी व विभिन्न प्रकार के खनिज ईंधनों (पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल आदि) की भट्टियों, कारखानों, बिजलीघरों, मोटरगाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाई-ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल तथा अन्य यौगिकों के सूक्ष्म कण प्रदूषक के रूप में वायु में मिल जाते हैं। मोटरगाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट (Automobile Exhaust) को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी माना गया है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें निकलती हैं। ये विषैली गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके अन्य पदार्थ बनाती हैं, जो अत्यन्त हानिकारक होते हैं।
2. औद्योगिक अवशिष्ट – बड़े नगरों में कल-कारखानों से निकलने वाली अनेक गैसें, धातु के कण, विभिन्न प्रकार के फ्लुओराइड, कभी-कभी रेडियोसक्रिय पदार्थों के कण, कोयले के अज्वलनशील खनिज आदि वहाँ की वायु को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अनेक प्रकार के रसायन प्रयोग में लाये जाते हैं।
3. धातुकर्मी प्रक्रम – खान से निकाले गये खनिजों (अयस्कों) से धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। इस प्रक्रम से जो धूल व धुआं निकलता है, उसमें क्रोमियम, बेरीलियम, आर्सेनिक, बैनेडियम, जस्ता, सीसा, ताँबा आदि के कण होते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं।
4. कृषि रसायन – कीटों व खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फसलों पर जो रसायन (ऐल्ड्रीन, गैमेक्सीन आदि) छिड़के जाते हैं, उनमें से भी अनेक विषाक्त पदार्थ वायु में पहुँचते हैं, जो उसे विषाक्त कर देते हैं।
5. वृक्षों तथा वनों को काटा जाना – हरे पेड़-पौधे वायुमण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वायुमण्डल में इन गैसों का सन्तुलन बना रहता है। अतः वनस्पतियों द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है। आज हमने वनों तथा अन्य स्थानों के वृक्षों व झाड़ियों को अन्धाधुन्ध काटा है जिससे वायुमण्डल में उपस्थित गैसों का सन्तुलन बिगड़ गया है।
6. मृत पदार्थ – मरे हुए वनस्पति, जानवर या मनुष्य आदि वायुमण्डल में खुले छोड़ दिये जाएँ तो उन पर अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणु, जीवाणु व विषाणु उगेंगे जो वायु-प्रदूषण उत्पन्न करेंगे।
7. जनसंख्या विस्फोट – पर्यावरण प्रदूषण का यदि एक सबसे प्रमुख कारण देना हो तो हम जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की बात भी नहीं उठती। यह अनुमान किया जाता है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्य ने ही वायुमण्डल में 36 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। यह मात्रा दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है।
8. परमाणु ऊर्जा – परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनेक देश परमाणु विस्फोट कर रहे हैं और बहुत-से देश ऐसा करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस प्रयास के प्रक्रम में रेडियोसक्रिय पदार्थों को उठाने, चूरा करने, छानने, पीसने से कुछ वायु प्रदूषक (जैसे—यूरेनियम, बेरीलियम, क्लोराइड, आयोडीन, ऑर्गन, स्ट्रीशियम, सीजियम, कार्बन आदि) वायु में आ – मिलते हैं।
9. युद्ध – छोटे या बड़े देशों के मध्य जहाँ कहीं भी युद्ध होता है वहाँ का वातावरण गोलियाँ चलने, बम फटने एवं विषैले अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से दूषित हो जाता हैं।
प्रश्न 3
पर्यावरण को शुद्ध रखने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा उत्तर : प्रदेश सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं ? [2007]
या
पर्यावरण शुद्धि के लिए केन्द्र सरकार तथा उत्तर : प्रदेश सरकार ने कौन-से उपाय किए हैं? [2015]
उत्तर :
पर्यावरण को शुद्ध रखने के उपाय
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि मानव अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। वर्तमान समय में हमें न तो शुद्ध वायु, जल तथा भोजन मिल रहा है और न शुद्ध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वास्तव में, पर्यावरण के अशुद्ध होने से इस समस्या का जन्म हुआ है। अत: पर्यावरण को शुद्ध रखकर ही प्रदूषण की घातक समस्या का मुकाबला किया जा सकता है। पर्यावरण को निम्नलिखित उपायों द्वारा शुद्ध रखा जा सकता है
(क) वायु-प्रदूषण के उपाय – पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वायु-प्रदूषण है। वायु-प्रदूषण मनुष्य के जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। वायु-प्रदूषण सबसे अधिक परिवहन के साधनों, उद्योगों व वनों की कटाई से होता है। अतः वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि
1. भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ नगरीकरण और औद्योगीकरण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण पाने के लिए वायुमण्डल की जाँच कराना प्रथम आवश्यक कार्य है, जिससे कि प्रदूषण के संकेन्द्रण को सीमा से अधिक बढ़ने से रोका जा सके।
2. धुआँ उगलने वाले परिवहन के साधनों की वृद्धि को रोका जाए तथा परिवहन के धुएँ की माप धुआँ मीटरों से की जाए। मोटर-परिवहन एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए।
3. धुआँ उगलने वाली सरकारी व गैर-सरकारी गाड़ियों के लाइसेन्स तुरन्त जब्त कर लिये जाएँ और उन्हें शिकायत दूर करने और पूरी जाँच के बाद ही दोबारा प्रमाण-पत्र दिया जाए। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए।
4. पर्यावरण में सन्तुलन बनाये रखने एवं वायु-प्रदूषण को दूर करने के लिए वन-क्षेत्र में वृद्धि की जाए तथा सामाजिक वानिकी को महत्त्व दिया जाए। इसके साथ-साथ वनों की अनियमित एवं अनियन्त्रित कटाई पर रोक लगायी जाए।
5. पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को नगरों के मध्य स्थापित करने की अनुमति न दी जाए। बड़े कल-कारखाने नगरों से दूर स्थापित कराए जाएँ तथा उनसे प्रदूषण मुक्त सभी आवश्यक शर्तों का कठोरता से पालन कराया जाए। इसके साथ ही कल-कारखानों से धुआँ उगलने वाली चिमनियों पर प्रदूषण-रोधक यन्त्र (फिल्टर) लगाना अनिवार्य किया जाए।
6. नगरों के मध्य कूड़ा-करकट, मल, व्यर्थ पदार्थ, औद्योगिक अवशिष्ट व अपमार्जक आदि न डाले जाएँ। उनका उपयोग विद्युत बनाने में कराया जाए।
7. भारत सरकार का वायु प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम, 1981, जो उत्तर : प्रदेश में भी लागू है, का कड़ाई से पालन कराया जाए।
(ख) जल-प्रदूषण के उपाय – पर्यावरण को अशुद्ध करने में जल-प्रदूषण भी सबसे बड़ी समस्या है। जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए –
ग्रामीण अंचल में –
- शौचालय तथा मल के गड्ढे खोदकर बनाये जाएँ।
- मल को नदियों व तालाबों में न बहाया जाए। इससे बेहतर खाद मिलेगा और जल-प्रदूषण की समस्या का स्वत: हल मिल जाएगा।
- कुओं पर जगत अवश्य बनायी जाए।
- जल को उबालकर तथा कुओं में दवाएँ डालकर शुद्ध किया जाए।
नगरीय क्षेत्रों में –
- जल संयन्त्रों से पानी साफ किया जाए और उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था की जाए।
- नदियों में कूड़ा-करकट, मल, व्यर्थ पदार्थ, औद्योगिक अवशिष्ट वे अपमार्जक न डाले जाएँ।
- नदियों में गिराये जाने वाले अवशिष्ट का उपचार किया जाए। प्रत्येक कारखाने पर औद्योगिक अवशिष्ट के लिए उपचार संयन्त्र लगाने की पाबन्दी लगायी जाए। इसके लिए कानून बनाये जाएँ और उनका कड़ाई से पालन कराया जाए।
- नदियों में अधजले शवों को बहाना रोका जाए और उनके लिए विद्युत शवदाह-गृहों का निर्माण किया जाए।
- देश में जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
- जल-प्रदूषण रोकने के लिए उसकी चौकसी एवं निगरानी के लिए समितियाँ गठित हों, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी, प्रदूषण निरोधक समितियों के सदस्य तथा प्रदूषित क्षेत्रों के नागरिक होने चाहिए।
- जन-सामान्य को इस समस्या के प्रति जाग्रत किया जाए और उनकी सक्रिय साझेदारी प्राप्त की जाए।
- नदियों में पशुओं को ने नहलाया जाए तथा नदी इत्यादि में वस्त्रों की धुलाई पर रोक लगायी जाए।
- कुओं को ढककर रखा जाए तथा ढके हुए नल लगाकर पेयजल की व्यवस्था की जाए।
- नगरों में पेयजल का वितरण जल को शुद्ध करके किया जाए।
(ग) ध्वनि-प्रदूषण के उपाय – पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण भी प्रदूषित कर रहा है। ध्वनिप्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं
- वायुयानों, रेलों, बसों, कारों, स्कूटरों एवं मोटर साइकिलों आदि में शोर-शमन यन्त्र (साइलेंसर) ठीक काम करते हैं या नहीं इसकी पूरी देख-रेख की जाए। जहाँ ये ठीक काम न कर रहे हों वहाँ इनका सड़क पर चलना तुरन्त बन्द कराया जाए और इस व्यवस्था को न मानने वालों को दण्डित किया जाए।
- विदेशों की भाँति व्यर्थ एवं अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना रोका जाए। अनिवार्य स्थिति में ही हॉर्न बजाने की अनुमति हो। शहरों में ‘खामोश क्षेत्र घोषित किया जाए।
- कल-कारखाने व रेलवे स्टेशन आदि आवासीय क्षेत्रों से बाहर स्थापित कराए जाएँ तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों के प्रयोग को सीमित किया जाए।
- वाद्य-यन्त्रों व लाउडस्पीकरों आदि के प्रयोग तथा उनकी तीव्र ध्वनि को नियन्त्रित एवं प्रतिबन्धित किया जाए।
(घ) अन्य उपाय-
- पर्यावरण को अशुद्ध करने में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी मुख्य कारण है। अतः जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण किया जाए।
- प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरणीय कारकों के सन्तुलन को सीमा से अधिक बिगाड़ने पर भारी क्षति उठानी पड़ती है। वनों की अन्धाधुन्ध कटाई को रोका जाए।
- नगरीकरण के विस्तार को रोका जाए।
- पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार एवं जागृति जन-मानस में की जाए।
- उद्योग एवं नगर के विकास में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी नीति का समावेश किया जाए।
- प्राकृतिक संसाधनों का शोषण योजनाबद्ध ढंग से किया जाए।
- पर्यावरण सन्तुलन को बिगड़ने से बचाया जाए।
- पर्यावरण सुरक्षा के नियम अधिक कठोर बनाये जाएँ।
पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्र
सरकार द्वारा किये गये प्रयास
पर्यावरण को शुद्ध रखने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं
- जल-प्रदूषण निवारण के लिए केन्द्र सरकार ने जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 बनाया है।
- केन्द्र सरकार ने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सन् 1986 में एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत ‘गंगा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन किया गया लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की योजना बनायी जिससे नयीं सीवर लाइन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण कराया गया। कारखानों के मालिकों को औद्योगिक अवशिष्ट उपचार के यन्त्र लगाने को कहा गया।
- भारत की अन्य नदियों; जैसे यमुना, गोमती तथा अन्य प्रदेशों; जैसे केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान की कुछ नदियाँ, जो प्रदूषित हो गयी हैं; को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी योजना बनायी गयी, जिसके अन्तर्गत विद्युत शवदाह-गृहों का निर्माण, कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में न गिराना आदि कार्यों पर बल दिया गया।
- परमाणु अस्त्रों को परीक्षण जो समुद्र में किया जाता है, उसको सीमित एवं नियन्त्रित करना।
- वायु-प्रदूषण हेतु वायु-प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम, 1981 बनाया हुआ है। वायु-प्रदूषण पर नियन्त्रण करने के लिए मोटर परिवहन ऐक्ट, नूयी औद्योगिक नीति एवं 1978 ई० में घोषित देश की नवीन वन नीति में पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्रफल में वृद्धि एवं वनों की अनियमित एवं अनियन्त्रित कटाई को रोकना आदि पर विशेष बल दिया गया है।
- शुद्ध पर्यावरण बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार ने पर्यावरण मन्त्रालय की स्थापना की हुई है, जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है।
- केन्द्र सरकार को परिवार कल्याण मन्त्रालय’ जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दे रहा
है, जिससे प्रदूषण की समस्या हल हो सके, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का महत्त्वपूर्ण कारण तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। - सन् 1985 में बहुप्रतिष्ठित कार्य योजना ‘गंगा एक्शन प्लान’ प्रारम्भ की गयी, जिसमें है 261 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया गया था। गंगा की योजना के दूसरे चरण हेतु केन्द्र सरकार ने 421 करोड़ स्वीकृत किये थे। इस योजना के अन्तर्गत यमुना, गोमती तथा दामोदर नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है। उक्त योजना जून, 1993 से प्रारम्भ की गयी
थी, साथ ही राज्य सरकारों से योजना को कार्यरूप प्रदान करने हेतु कहा गया था।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा के यमुना नगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गाँव, फरीदाबाद; उत्तर : प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, वृन्दावन, आगरा, इटावा, लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर और दिल्ली में यमुना नदी, हिंडन तथा गोमती नदियों की सफाई के लिए योजनाएँ चलाई जाती हैं।
9. वायु-प्रदूषण नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय नियन्त्रण बोर्ड ने 1993 ई० तक देश के 92 प्रमुख नगरों में वायु गुणवत्ता की नियमित चेकिंग के लिए 290 स्टेशन स्थापित किये हैं।
नयी रणनीति – पहली बार सरकार ने बढ़ते वाहन-प्रदूषण को रोकने के लिए नयी रणनीति बनायी है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं|
- वाहन उत्सर्जन मानक कड़े बनाये गये थे जिन्हें दो चरणों में सन् 1996 व 2000 ई० से लागू करने का प्रस्ताव था।
- वाहन-प्रदूषण को कम करने के लिए लेड मुक्त पेट्रोल, कैटालिटिक कन्वर्टर व कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी० एन० जी०) के पहलुओं पर तेजी से विचार किया गया है।
पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने के लिए उत्तर : प्रदेश सरकार
द्वारा किये गये प्रयास
पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने के लिए उत्तर : प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किये हैं
1. उत्तर प्रदेश शासन ने पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने तथा उसके निदान के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी निदेशालय की स्थापना की।
2. शासन को पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्बन्धी परामर्श देने के लिए मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया गया है। इसके सदस्य विभिन्न विभागों से सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा मन्त्रिगण हैं। इस बोर्ड को जलवायु एवं मिट्टी के प्रदूषण, खनन, वातावरण की गन्दगी, नये उद्योगों की स्थापना, शहरों का विकास, ऐतिहासिक इमारतों की प्रदूषण से सुरक्षा इत्यादि कार्य निर्दिष्ट किये गये हैं। यह बोर्ड पर्यावरण सम्बन्धी ऐसे नीति-निर्धारण में शासन को आवश्यक परामर्श भी देता है जो विकास कार्यों के तालमेल में हो। इस बोर्ड तथा इसकी कार्यकारिणी समिति ने शासन को कई परामर्श दिये हैं, जिन पर सरकार कार्य कर रही है, जिनमें से निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं
- विकास विभागों की वृहत् योजनाओं का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सन्तुलन की दृष्टि से पर्यवेक्षण किया जाए।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सन्तुलन हेतु वर्तमान अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किया जाए।
- उद्योग एवं नगर विकास में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी नीति का समावेश किया जाए।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी निदेशालय द्वारा प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वृहत् कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग निम्नवत् हैं
(क) भूमि एवं जल प्रबन्ध।
(ख) प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक इमारतों, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों का संरक्षण।
(ग) पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण।
(घ) मानव बस्ती।
(ङ) पर्यावरणीय शिक्षा एवं तत्सम्बन्धी ज्ञान की जन-मानस में जागृति।
(च) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नियमों एवं अधिनियमों में संशोधन।
संक्षेप में, प्रदेश सरकार पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपर्युक्त सभी कार्य कर रही है। भारत सरकार का वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 जो अपने प्रदेश में भी लागू है, वायु-प्रदूषण पर नियन्त्रण कर रहा है। इसी प्रकार जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 बना हुआ है, जो जल-प्रदूषण पर नियन्त्रण कर रहा है। प्रदेश में मोटर परिवहन ऐक्ट भी लागू है, जो धुआँ उगलने वाले एवं शोर करने वाले परिवहनों पर नियन्त्रण करके पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक है। पर्यावरण को शुद्ध रखने एवं पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग, उत्तर : प्रदेश कार्यरत है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)
प्रश्न 1
प्रदूषण के चार प्रकार बताइए। [2007, 11, 13]
उत्तर :
वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के पाँच प्रकार बताये हैं, जिनमें से चार निम्नलिखित हैं
1. वायु-प्रदूषण – वायु जीवन का एक प्रमुख तत्त्व है, जो सभी प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन के लिए परम आवश्यक है। वायुमण्डल में हाइड्रो-कार्बनिक गैसों, विषैले धूलकणों तथा कल-कारखानों से निकलने वाले धुएँ के कारण जब वायु में हानिकारक तत्त्व बढ़ जाते हैं तो वायु का प्राकृतिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। इसे वायु-प्रदूषण कहते हैं।
2. जल-प्रदूषण – अनेक भौतिक, प्रौद्योगिक तथा मानवीय कारणों से जब जल का रूप प्राकृतिक नहीं रह जाता तथा उसमें गन्दे पदार्थों तथा विषाणुओं का समावेश हो जाता है, उसे जल-प्रदूषण कहते हैं।
3. ध्वनि-प्रदूषण – वातावरण में बहुत तेज और असहनीय आवाज से जो शोर उत्पन्न होता है, वही ध्वनि-प्रदूषण कहलाता है। शोर से उत्पन्न होने वाले इस प्रदूषण ने बड़े शहरों में। विकराल रूप धारण कर लिया है। मृदा-प्रदूषण-मृदा की रचना विभिन्न तरीके के लवण, गैस, खनिज पदार्थ, जल, चट्टानों एवं जीवाश्म आदि के मिश्रण से होती है। इन पदार्थों के अनुपात में जब हानिकारक परिवर्तन होने लगता है, तो उसी दशा को मृदा-प्रदूषण कहा जाता है। इसका मुख्य कारण। कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता हुआ प्रयोग है।
प्रश्न 2
जल-प्रदूषण की रोकथाम के सन्दर्भ में ‘अवशिष्ट जल के उपचार’ एवं ‘पुनः चक्रण का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
अवशिष्ट जल का उपचार – कल-कारखानों के अवशिष्ट जल को नदी में भेजने से पहले उसका उपयुक्त उपचार करना आवश्यक होता है जिससे प्रदूषक नदी, झील या तालाब के जल को प्रदूषित न कर सकें, क्योंकि हमारे वाटर वर्ल्स इन्हीं से जल लेकर हमें पीने को देते हैं। सीवर के जल को भी शहर के बाहर दोषरहित बनाकर ही नदियों में छोड़ना चाहिए। कारखानों के जल से विषैले पदार्थ को ही नहीं बल्कि ऊष्मा को निकालकर ही उसे नदी में डालना चाहिए।
पुनः चक्रण – शहरी और औद्योगिक गन्दे जल को नदियों में मिलाने से पहले साफ करना और निथारना एक बड़ा खर्चीला काम है। अत: ठोस अवशिष्ट पदार्थों; जैसे-कूड़ा-करकट, सीवेज (मल-मूत्र) और अवशिष्ट जल से रासायनिक विधियों द्वारा अन्य उपयोगी पदार्थ बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार हानि को लाभ में बदला जा सकता है। उदाहरणार्थ-पटना में मल-मूत्र व गन्दे जल से बायोगैस बन रही है जिससे पूरा मुहल्ला प्रभावित हो रहा है। बंगलुरू शहर में भी प्रदूषित जल से बायोगैस बनायी जा रही है।
प्रश्न 3
कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमण्डल में बढ़ता प्रवाह किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा है ? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
वायुमण्डल को प्रदूषित करने में वाहनों से छोड़े जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रमुख हाथ है। नगरों में बसों, मोटरों, ट्रकों, टैम्पों तथा स्कूटर-मोटर साइकिलों से इतना अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड धुआँ निकलता है कि सड़क पर चलने वाले लोगों का दम घुटने लगता है। यही कारण है कि बड़े नगरों में लोग विशेषकर बच्चे, श्वास रोगों से पीड़ित पाये जाने लगे हैं। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न करती है।
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के अतिरिक्त, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा है
1. पारिवारिक विघटन कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पर्यावरण प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को विघटित करने वाला एक प्रमुख स्रोत है। जैसे-जैसे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इससे परिवार में आर्थिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं तथा आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्तियों में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। परिवार के सदस्यों में सम्बन्ध मधुर नहीं रहते, बल्कि वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। धीरे-धीरे परिवार में बढ़ते हुए तनाव पारिवारिक विघटन का कारण बन जाते हैं।
2. अपराधों में वृद्धि-मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, वे सरलता से अपराधों की ओर बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि गाँव की अपेक्षा बड़े नगरों में अपराध की दर अधिक होती है।
प्रश्न 4
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु चार प्रमुख उपायों की विवेचना कीजिए।
उत्तर :
प्रदूषण नियन्त्रण हेतु चार प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं
- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के द्वारा केन्द्र और राज्य बोर्डो को पर्यावरण के अतिरिक्त उत्तर :दायित्व सौंपे गये हैं।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत जल का उपभोग करने वाले उद्योगों से उपकर वसूल किया जाता है। यह उपकर राज्यों को बाँटा जाता है।
- जल गुणवत्ता का मूल्यांकन-नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु 170 निगरानी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- राष्ट्रीय परिवेश वायु-गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क-ये केन्द्र वायु में व्याप्त धूल-कणों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के सम्बन्ध में वायु-गुणवत्ता की निगरानी करते हैं।
प्रश्न 5
ध्वनि-प्रदूषण क्या है ? इसके प्रकार बताइए। या शोर (ध्वनि) प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर :
कम्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अप्रिय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहा जाता है। तीखी ध्वनि या आवाज को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई डेसीबेल (decibel or dB) है जिसका मान 0 से लेकर 120 तक होता है। डेसीबेल पैमाने पर ‘शून्य’ ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहाँ से ध्वनि सुनाई देनी आरम्भ होती है। 85 से 95 डेसीबेल शोर सहने लायक और 120 डेसीबेल या उससे अधिक का शोर असह्य होता है।
ध्वनि-प्रदूषण के स्रोत – ध्वनि-प्रदूषण मुख्यत: दो प्रकार के स्रोतों से होता है-
1. प्राकृतिक स्रोत – बिजली की कड़क, बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएँ, ऊँचे स्थान से गिरता जल, आँधी, तूफान, ज्वालामुखी का फटना एवं उच्च तीव्रता वाली जल-वर्षा।
2. कृत्रिम स्रोत – ये स्रोत मानवजनित हैं; उदाहरणार्थ-मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला शोर, वायुयान, रेलगाड़ी तथा उसकी सीटी से होने वाला शोर, लाउडस्पीकर एवं म्यूजिक सिस्टम से होने वाला शोर, टाइपराइटर की खड़खड़ाहट, टेलीफोन की घण्टी आदि से होने वाला शोर।।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)
प्रश्न 1
संक्षेप में बताइए कौन-सी वस्तुएँ हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं ?
उत्तर :
संक्षेप में, जिस मिट्टी में पेड़-पौधे उगते और बढ़ते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो पानी हम सब पीते हैं, जिस हवा में साँस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं और जिन वस्तुओं को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, वे सब वस्तुएँ हमारे लिये पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
प्रश्न 2
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं ? [2010]
उत्तर :
पर्यावरण के घटकों; जैसे-वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक है, दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे माल के साधनों को हानि पहुँचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।
प्रश्न 3
प्रदूषण के चार कुप्रभाव बताइए। [2015, 16, 17]
उत्तर :
- वायु-प्रदूषण का कुप्रभाव-ओजोन-परत में छेद होने की सम्भावना से सारा विश्व भयाक्रांत हो उठा है।
- जल-प्रदूषण के कुप्रभाव-जल-प्रदूषण से अनेक बीमारियाँ; जैसे-हैजा, पीलिया, पेट में कीड़े, टायफाइड फैलती हैं।
- ध्वनि-प्रदूषण का कुप्रभाव-यह प्रदूषण मानव के कानों के परदों पर, मस्तिष्क और शरीर पर इतना घातक आक्रमण करता है कि विश्व के सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक इससे चिन्तित हैं।
- मृदा-प्रदूषण का कुप्रभाव–दूषित मृदा में रोगों के जीवाणु पनपते हैं जिनसे मनुष्यों और अन्य जीवों में रोग फैलते हैं।
प्रश्न 4
प्रदूषण रोकने में वृक्षारोपण की भूमिका बताइए।
उत्तर :
वृक्षारोपण और वनों को लगाने से वायुमण्डल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का सन्तुलन नहीं बिगड़ता। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि यदि आबादी का 23% वन हों तो वायु-प्रदूषण से हानि नहीं पहुँचती है। वनों का काटा जाना तत्परता से रोका जाना चाहिए। ऐसे कानून बनाये जाने चाहिए जिनसे वनोन्मूलन को दण्डनीय अपराध करार दिया जा सके।
प्रश्न 5
जल-प्रदूषण के क्या कारण हैं?
उत्तर :
औद्योगीकरण, नगरीकरण, समुद्रों में अस्त्रों का परीक्षण, नदियों में अधजले शवों, जानवरों की लाश व अस्थि-विसर्जन करना, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का जल में मिलना, घरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार से दूषित जल का जलाशयों व नदियों आदि में मिलना जलप्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।
प्रश्न 6
जल-प्रदूषण से किन-किन रोगों के होने की सम्भावना रहती है ?
उत्तर :
प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक रोगों के होने की सम्भावना रहती है; जैसे-पक्षाघात, पोलियो, पीलिया (Jaundice), मियादी बुखार (Typhoid), हैजा, डायरिया, क्षय रोग, पेचिश, इन्सेफेलाइटिस, कन्जंक्टीवाइटिस आदि। यदि जल में रेडियोसक्रिय पदार्थ और लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसी विषाक्त धातु हों तो कैंसर तथा कुष्ठ जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं। वर्ष 1988 में केवल दिल्ली में प्रदूषित जल सेवन से एक हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
प्रश्न 7
वायु-प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं अनियन्त्रित भवन-निर्माण, परिवहन के साधन (ऑटोमोबाइल), वनों का बड़ी मात्रा में कटान, रसोईघरों व कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ तथा युद्ध, आणविक विस्फोट एवं दहन की क्रियाएँ आदि वायु प्रदूषण के कारण हैं।
प्रश्न 8
वायु-प्रदूषण निराकरण के कोई चार उपाय बताइए।
उत्तर :
वायु प्रदूषण निराकरण के चार उपाय निम्नलिखित हैं|
- परिवहन के साधनों पर धुआँ रहित यनत्र लगाना।
- बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करना।।
- रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को नियन्त्रित करना।
- घरों में बायोगैस, पेट्रोलियम गैस या धुआँ रहित चूल्हों का प्रयोग करना।
प्रश्न 9
प्राकृतिक प्रदूषक से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर :
कुछ प्रदूषक; जैसे-परागकण, कवक, निम्नतर पौधों के बीजाणु, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसें, मार्श गैस, तटीय प्रदेश में नमक के अत्यन्त सूक्ष्म कण आदि प्राकृतिक रूप में वायु में आ मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। इन्हें प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं।
प्रश्न 10
प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोक्साइड का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
मोटरगाड़ियों, औद्योगिक संयन्त्रों, घर के चूल्हों तथा सिगरेट के धुएँ से कार्बन मोनोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलती हैं, जो श्वसन की क्रिया में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के उचित संचरण के कार्य को रोक देती हैं। शरीर की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, थकान, सिरदर्द, काम करने की अनिच्छा, दृष्टि-संवेदनशीलता में कमी तथा हृदय व रक्त-संचार में शिथिलता आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इन गैसों (विशेषकर CO) की अधिकता से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है।
प्रश्न 11
‘जनसंख्या विस्फोट कैसे प्रदूषक है ?
उत्तर :
पर्यावरण प्रदूषण का यदि एक सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो नि:सन्देह जनसंख्या विस्फोट को माना जा सकता है। यदि संसार की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं हुई होती तो आज प्रदूषण की बात भी नहीं उठती। यह अनुमान किया जाता है कि गत 100 वर्षों में केवल मनुष्य ने ही वायुमण्डल में 36 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। यह मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
निश्चित उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1
प्रदूषण से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर :
जब पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो जाता है और निर्भरता नष्ट हो जाती है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं।
प्रश्न 2
प्रदूषक किसे कहते हैं ?
उत्तर :
जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है, उन्हें प्रदूषक कहते हैं; जैसे-धूल, धुआँ।
प्रश्न 3
पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम कब बना था ?
उत्तर :
पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 ई० में बना था।
प्रश्न 4
भारत में पानी के मुख्य स्रोत क्या हैं ?
उत्तर :
भारत में पानी के मुख्य स्रोत कुएँ, तालाब, झरने और नदियाँ हैं।
प्रश्न 5
समुद्रों में प्रदूषण कैसे होता है ?
उत्तर :
समुद्रों में जहाजरानी, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण, समुद्र में फेंकी गयी गन्दगी, मल-विसर्जन एवं औद्योगिक अवशिष्टों के विषैले तत्त्वों के कारण समुद्री जल निरन्तर प्रदूषित होता रहता है।
प्रश्न 6
जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम कब बना था ?
उत्तर :
जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 ई० में बना था।
प्रश्न 7
वायु-प्रदूषण क्या है ?
उत्तर :
वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों का वह परिवर्तन जो मानव व उसके लाभदायक जीवों व वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वायु-प्रदूषण कहलाता है।
प्रश्न 8
ओजोन परत क्या है और इसकी क्या महत्ता है ?
उत्तर :
ओजोन परत पृथ्वी का ऐसा रक्षा-कवच है जो सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिण्डों से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है।
प्रश्न 9
स्वचालित वाहनों से कौन-सी गैस निकलती है ?
उत्तर :
स्वचालित वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है।
प्रश्न 10
भारत में सर्वाधिक ध्वनि-प्रदूषण वाला नगर कौन-सा है ?
उत्तर :
मुम्बई भारत का सर्वाधिक ध्वनि-प्रदूषण वाला नगर है।
प्रश्न 11
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है ?
उत्तर :
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसीबेल है।
प्रश्न 12
‘मानव परमाणु शक्ति के योग्य नहीं है।’ यह कथन किसका है ?
उत्तर :
यह कथन अलबर्ट आइन्सटाइन का है।
प्रश्न 13
प्रदूषण की श्रृंखला में सबसे बड़ा अभिशाप क्या और क्यों है ?
उत्तर :
परमाणु की श्रृंखला में रेडियोधर्मी-प्रदूषण सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि परमाणु रिऐक्टरों में आणविक प्रक्रमों से बचे कचरे को नष्ट करना एक समस्या है।
प्रश्न 14
रेडियोधर्मी-प्रदूषण को कम करने का क्या तरीका है ?
उत्तर :
रेडियोधर्मी-प्रदूषण को कम करने तरीका है कि परमाणु ऊर्जा की होड़ विश्व में समाप्त कर दी जाए।
प्रश्न 15
चिपको आन्दोलन का प्रणेता कौन है ? [2013, 15]
उत्तर :
सुन्दरलाल बहुगुणा चिपको आन्दोलन के प्रणेता हैं।
प्रश्न 16
चिपको आन्दोलन किससे सम्बन्धित है ? [2014]
उत्तर :
चिपको आन्दोलन वन-संरक्षण से सम्बन्धित है।
प्रश्न 17
प्रदूषण के चार प्रमुख प्रकार बताइए। [2015, 16, 17]
उत्तर :
- जल-प्रदूषण,
- वायु-प्रदूषण,
- ध्वनि-प्रदूषण तथा
- मृदा-प्रदूषण।
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अक)
1. विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ?
(क) 5 जून को
(ख) 24 अक्टूबर को
(ग) 24 जनवरी को
(घ) 15 अगस्त को
2. सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है|
(क) ऑक्सीजन परत
(ख) वायु में उपस्थित जल-कण
(ग) वायु में उपस्थित धूल-कण
(घ) ओजोन परत
3. प्रदूषण की श्रृंखला में सबसे बड़ा अभिशाप है [2013]
(क) मृदा प्रदूषण
(ख) ध्वनि प्रदूषण
(ग) रेडियोधर्मी प्रदूषण
(घ) जल प्रदूषण
4. मानव समाज में रोगों का कारण है [2013]
(क) प्रदूषित भोजन
(ख) प्रदूषित वायु
(ग) प्रदूषित जल
(घ) ये सभी
उत्तर:
- (क) 5 जून को,
- (घ) ओजोन परत,
- (ग) रेडियोधर्मी प्रदूषण,
- (घ) ये सभी
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sociology Chapter 2 Concept of Pollution Causes, Social Effects and Solution (प्रदूषण की अवधारण: कारण, सामाजिक प्रभाव और निराकरण), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.