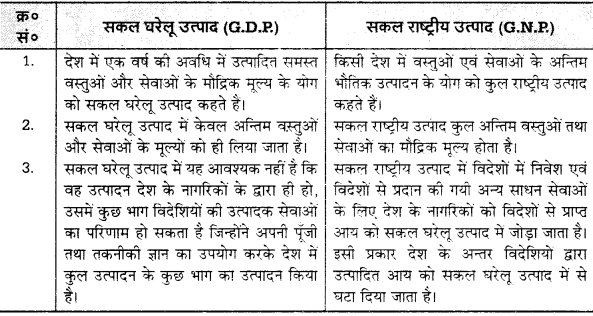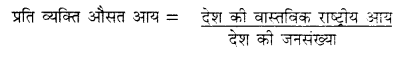UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 17 Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat (भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत) are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 17 Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat (भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत).
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Civics |
| Chapter |
Chapter 17 |
| Chapter Name |
Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat
(भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत) |
| Number of Questions Solved |
50 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 17 Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat (भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत)
विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1.
भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना का उल्लेख कीजिए। उसे संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? [2010]
या
“भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक व नागरिकों के मूलाधिकारों का रक्षक कहा जाता है।” व्याख्या कीजिए। [2014]
या
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? [2014]
या
सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन कीजिए। उसको ‘संविधान का रक्षक’ एवं ‘नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक’ क्यों कहा जाता है ? [2008, 10, 12, 14, 15]
या
उच्चतम न्यायालय का संगठन समझाइए। उसके महत्त्व को भी समझाइए। [2008, 10, 12, 13]
या
भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन व उसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। [2010]
या
न्यायालय की स्वतन्त्रता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता (महत्त्व)
भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत में संविधान वे लोकतन्त्र की रक्षा का दायित्व किसे सौंपा जाए? गम्भीर विचार-विमर्श के पश्चात् संविधाननिर्माताओं ने भारत संघ में लोकतन्त्र, नागरिकों के अधिकार व संविधान की रक्षा का दायित्व एक स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को सौंपा। भारत में न्याय-व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। श्री वी० एस० देशपापडे के शब्दों में, “भारत में संविधान व लोकतन्त्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का ही है। स्वतन्त्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकरण बहुत गौरवमय रहा है तथा आम जनता में व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों तथा स्वाधीनता के प्रहरी के रूप में उसके प्रति अटूट श्रद्धा-विश्वास है।
भारत की संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायालय की आवश्यकता अथवा महत्त्व को निम्नलिखित तर्को द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है –
1. संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य – संघीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र को लेकर केन्द्र व राज्यों में विवाद की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। अतः केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद के निराकरण हेतु एक स्वतन्त्र व निष्पक्ष शक्ति का होना अनिवार्य होता है। भारत में इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए एक स्वतन्त्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है। जी० एन० जोशी ने संघीय व्यवस्था में निष्पक्ष व स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि “संघात्मक शासन में कई सरकारों का समन्वय होने के कारण संघर्ष अवश्यम्भावी है। अतः संघीय नीति का यह आवश्यक गुण है कि देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो, जो संघीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका तथा इकाइयों की सरकारों से स्वतन्त्र हो।’
2. संविधान का रक्षक – भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गयी है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाये रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपनी इस शक्ति के आधार पर वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या उसी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है।
3. परामर्शदात्री संस्था के रूप में – भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँग सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है। कि न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने या न करने के लिए राष्ट्रपति पूर्ण स्वतन्त्र होता
4. मौलिक अधिकारों का रक्षक – संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है कि न्यायालय : संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इस सम्बन्ध में पायली ने कहा है कि “मौलिक अधिकारों का महत्त्व एवं सत्ता समय-समय पर न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों से सिद्ध होती है, जिससे कार्यपालिका की निरंकुशता तथा विधानमण्डलों की स्वेच्छाचारिता से नागरिकों की रक्षा होती है।”
5. भारत का अन्तिम न्यायालय – भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय अन्तिम न्यायालय है। परिणामस्वरूप इसके निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होते हैं। इन निर्णयों में परिवर्तन केवल वह ही कर सकता है।
अन्तत: सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता व महत्त्व को डॉ० एम० वी० पायली के इस कथन से प्रमाणित किया जा सकता है कि ‘‘सर्वोच्च न्यायालय संघीय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। यह संविधान की व्याख्या करने वाला, केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण करने वाला तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अन्तिम अभिकरण है।”
सर्वोच्च न्यायालय का गठन
संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा-शर्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। अनुच्छेद 124 के अनुसार, “भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश होंगे।” परन्तु इस सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। वर्तमान समय में 1985 ई० में पारित विधि के अन्तर्गत संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गयी है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
न्यायाधीशों की योग्यताएँ (मुख्य न्यायाधीश) – संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं –
- वह भारत का नागरिक हो।
- वह कम-से-कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो अथवा वह दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की दृष्टि में विख्यात विधिवेत्ता हो।
- उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो।
कार्यकाल – उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, परन्तु यदि न्यायाधीश समय से पूर्व पदत्याग करना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर मुक्त हो सकता है।
महाभियोग – संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाकर, राष्ट्रपति के माध्यम से पदच्युत किया जा सकता है।
शपथ – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद को ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है।
वेतन व भत्ते – नवीन वेतनमानों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 मासिक वेतन व अन्य न्यायाधीशों को र 90,000 रुपये मासिक वेतन की धनराशि देना निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए नि:शुल्क आवास व सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पेंशन देने की व्यवस्था भी की गयी है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि में से दिये जाते हैं, जो संसद के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होना है। इसके साथ ही न्यायाधीशों के वेतन में उनके कार्यकाल के समय में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल वित्तीय आपात के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनभत्ते कम किये जा सकते हैं।
उन्मुक्तियाँ – संविधान द्वारा न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ निम्नलिखित हैं –
- न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों को आलोचना से मुक्त रखा गया है।
- किसी भी निर्णय के सम्बन्ध में न्यायाधीश पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने वह निर्णय स्वार्थवश तथा किसी के हित विशेष को ध्यान में रखकर लिया है।
- महाभियोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीश के आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं की जा सकती।
वकालत पर रोक – जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन हो जाता है, वह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। संविधान द्वारा यह व्यवस्था न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल में निष्पक्ष व स्वतन्त्र होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर की गयी है।
[संकेत – उच्चतम न्यायालय के कार्य व क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय की स्वतन्त्रता का संरक्षण हेतु विस्तृत प्रश्न 2 का अध्ययन करें]
प्रश्न 2.
उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
या
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किस प्रकार के लेख (रिट) जारी कर सकते हैं? किन्हीं दो का उदाहरण देते हुए समझाइए। [2012]
या
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए और यह भी बताइए कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? [2016]
या
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। [2010, 12]
या
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। [2013, 14, 15, 16]
या
न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएँ की गयी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। [2013]
या
सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। [2013]
या
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता का संरक्षण किस प्रकार किया गया है? [2014]
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोपरि न्यायालय है। अतएव उसे अत्यधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन अधिकारों को निम्नलिखित सन्दर्भो में समझा जा सकता है –
(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
श्री दुर्गादास बसु ने कहा कि “यद्यपि हमारा संविधान एक सन्धि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्य या राज्यों के बीच न्याय-योग्य विवादों के निर्णय का प्रारम्भिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है।’
इस क्षेत्राधिकार को पुनः दो वर्गों में रखा जा सकता है –
(अ) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार – प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे अधिकार आते हैं जो उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय कुछ उन विवादों पर विचार करता है जिन पर अन्य न्यायालय विचार नहीं कर सकते हैं। ये विवाद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –
- भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- वे विवाद जिनमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक ओर हों और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर हों।
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 26 जनवरी, 1950 के पूर्व जो सन्धियाँ अथवा संविदाएँ भारत संघ और देशी राज्यों के बीच की गयी थीं और यदि वे इस समय भी लागू हों तो उन पर उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।
(ब) प्रारम्भिक समवर्ती क्षेत्राधिकार – भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही उच्च न्यायालयों को भी प्रदान कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही करे।
(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार
भारत में एकीकृत न्यायिक-प्रणाली अपनाने के कारण राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं और इस रूप में उसका इन उच्च न्यायालयों पर अधीक्षण और नियन्त्रण स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा, केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को अग्रलिखित वर्गों में रखा जा सकता है –
(क) संवैधानिक अपीलें – संवैधानिक मामलों से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तब की जा सकती है जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में “संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि का कोई सारवान प्रश्न सन्निहित है।’ लेकिन यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देता है तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि उसमें कानून का कोई सारवान प्रश्न सन्निहित है। निर्वाचन आयोग बनाम श्री वेंकटराव (1953) के मुकदमे में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी संवैधानिक विषय में अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है अथवा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका उत्तर ‘हाँ’ में दिया है।
(ख) दीवानी की अपीलें – संविधान द्वारा दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील सुने जाने की व्यवस्था की गयी है। किसी भी राशि का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सुनने योग्य है या उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि मुकदमे में कोई कानूनी प्रश्न विवादग्रस्त है। यदि उच्च न्यायालय किसी दीवानी मामले में इस प्रकार का प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी किसी व्यक्ति को अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
(ग) फौजदारी की अपीलें – फौजदारी के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ये अपीलें इन दशाओं में की जा सकती हैं –
- जब किसी उच्च न्यायालय ने अधीन न्यायालय के दण्ड-मुक्ति के निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
- जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि विवाद उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने योग्य है।
- जब किसी उच्च न्यायालय के किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से मँगाकर अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया हो।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे में यह अनुभव करता है कि किसी व्यक्ति के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, तो वह सैनिक न्यायालयों के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।
(घ) विशिष्ट अपील – अनुच्छेद 136 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने विवेक से प्रभावित पक्ष को अपील का अधिकार प्रदान करे। किसी सैनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय दण्ड या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है, चाहे भले ही उच्च न्यायालय ने अपील की आज्ञा से इन्कार ही क्यों न किया हो।
अपीलीय क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लक्ष्य करते हुए ही 1950 ई० को सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए श्री एम० सी० सीतलवाड ने कहा था कि “यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप व विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य-क्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक हैं।”
(3) संविधान का रक्षक व मूल अधिकारों का प्रहरी
संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में स्पष्टीकरण देकर उचित व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या को अन्तिम तथा सर्वोच्च माना जाता है। केवल संविधान की व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि इसकी रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन करने का भी अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका को कोई आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून व आदेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता कायम रखता है।
संविधान की धारा 32 के अनुसार न्यायालय का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे। इन अधिकारों की रक्षा के लिए यह न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख जारी करता है।
(4) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। अनुच्छेद 143 के अनुसार, यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्यों के बारे में कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया। गया है या उठने वाला है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना जरूरी है तो वह उस प्रश्न को परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है, किन्तु अनुच्छेद 143 ‘बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है। यह न तो राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वह सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर न्यायालय की राय माँगे और न ही सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य करता है कि वह भेजे गये प्रश्न पर अपनी राय दे। वैसे भी यह राय ‘न्यायिक उद्घोषणा’ या ‘न्यायिक निर्णय नहीं है। इसीलिए इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से अनेक बार परामर्श माँगा है। केरल शिक्षा विधेयक, 1947′ में, ‘राष्ट्रपति के चुनाव पर एवं 1978 ई० में विशेष अदालत विधेयक पर माँगी गयी सम्मतियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण रही हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने या उसे कम करने में सहायक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा सलाहकार की भूमिका अदा करना पसन्द नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत की व्यवस्था कनाडा और बर्मा के अनुरूप है।।
(5) अन्य क्षेत्राधिकार
(अ) अधीनस्थ न्यायालयों की जाँच – सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।
(ब) न्यायालयों की कार्यवाही संचालन हेतु नियम बनाना – सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने हेतु नियम बनाने का अधिकार है, परन्तु उन नियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है।
(स) पुनर्विचार का अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय यदि ऐसा अनुभव करे कि वह अपने निर्णय में कोई भूल कर बैठा है या उसके निर्णय में कोई कमी रह गयी है, तो उस विवाद पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले निर्णय को बदलकर अनेक बार नये निर्णय दिये हैं।
(6) अभिलेख न्यायालय
अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसके दो अर्थ हैं –
(i) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और अदालती कार्यवाही को अभिलेख के रूप में रखा जाएगा जो अधीनस्थ न्यायालयों में दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये जाएँगे और उनकी प्रामाणिकता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जाएगा।
(ii) इस न्यायालय द्वारा ‘न्यायालय की अवमानना’ के लिए दण्ड दिया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में स्वतः ही मान्य हो जाती है, लेकिन संविधान में इस न्यायालय की अवमानना करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था विशिष्ट रूप से की गयी है।
सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना ही है। इस सम्बन्ध में श्री डी० के० सेन ने लिखा है, ‘न्यायालय भारत के सभी न्यायालयों के न्यायिक निरीक्षण की शक्तियाँ रखता है और वही संविधान का वास्तविक व्याख्याता और संरक्षक है। उसका यह कर्त्तव्य होता है कि वह यह देखे कि उसके प्रावधानों को उचित रूप में माना जा रहा है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ वह उसके प्रावधानों को स्पष्ट करता है।”
संक्षेप में, मौलिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ ‘विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हैं।” इस पर भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि इसकी शक्तियाँ ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कारण मर्यादित हैं, इसीलिए यह संसद के तीसरे सदन की भूमिका नहीं अपना सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं –
- न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से पृथक् कर दिया गया है।
- न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की संचित निधि से दिये जाते हैं। न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गयी है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है।
- न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। यद्यपि महाभियोग लगाकर न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, परन्तु वह बहुत जटिल है; इसलिए न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना भी सरल नहीं है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस कारण न्यायाधीश पूर्ण स्वतन्त्र रहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णयों व कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती है। इस कारण भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली के संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार है।

प्रश्न 3.
उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के महत्त्व की विवेचना कीजिए। उदाहरण देकर समझाइए। [2009]
या
भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुरावलोकन के अधिकार का महत्त्व समझाइए। [2008, 2009]
या
संसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता से सम्बन्धित वाद-विवाद के सन्दर्भ में न्यायिक समीक्षा के सिद्धान्त का सावधानी से परीक्षण कीजिए। [2009]
या
संसद और न्यायालय की सर्वोच्चता से सम्बन्धित विवाद के सन्दर्भ में न्यायिक समीक्षा के सिद्धान्त का सावधानी से परीक्षण कीजिए। [2007]
या
न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। [2015]
या
भारत में न्यायिक समीक्षा के अर्थ एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए। [2011]
उत्तर :
न्यायिक पुनर्विलोकन (पुनरावलोकन) का अर्थ
भारत की न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान सभा को अमेरिकी संविधान-निर्माताओं की अनेक मौलिक देने हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान निर्माताओं द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह सौंपा गया है कि वह विधायिका तथा कार्यपालिका को नियन्त्रित करे। अमेरिका में संविधान सर्वोपरि है, इसलिए वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय यह जाँच करे कि वे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस अधिकार के अन्तर्गत यदि किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कोई कानून संघीय संविधान अथवा संयुक्त राज्य द्वारा की गई सन्धि के प्रतिकूल हो तथा कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रतिकूल हों तो संघीय न्यायपालिका उसे वैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन’ कहते हैं। कॉरविन के शब्दों में-“न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं, जिन्हें वे अवैधानिक और व्यर्थ समझे।”
न्यायिक पुनर्विलोकन का संचालन
भारत में भी उच्चतम न्यायालय को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समान ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में भी संविधान को सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। अतः न्यायपालिका का यह अधिकार व कर्तव्य है कि वह संसद अथवा विधानमण्डलों द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित कर दे जो संविधान की धाराओं का अतिक्रमण करते हों। आरत का उच्चतम न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure established by lawy) के आधार पर करता है जबकि अमेरिका का उच्चतम न्यायालय ‘कानून की उचित प्रक्रिया (Due procedure of law) के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय यह निश्चित करने में कि कोई कानून संवैधानिक है अथवा नहीं प्राकृतिक न्याय । के सिद्धान्तों को या उचित-अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता है।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने पिछले अनेक वर्षों में ऐसे दूरगामी निर्णय दिए हैं जिनमें न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग किया गया है; जैसे-‘गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम के 14वें खण्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया।
न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना
न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है।
1. मौलिक कार्यों के सम्पादन में कमी – कुछ आलोचकों का विचार है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार के कारण उच्चतम न्यायालय ने अपने मौलिक कार्यों की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया है। यह विवादों का निपटारा नहीं करता है वरन् इसका मुख्य कार्य सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में सहभागिता करना है। अब विधानमण्डल जनता की सामान्य इच्छा को विधि के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त नहीं कर सकता है।
2. न्यायाधीशों का संकीर्ण दृष्टिकोण – न्यायिक पुनर्विलोकन के विषय में हम इस बात को नकार नहीं सकते कि न्यायाधीश भी स्वाभाविक रूप से परम्परावादी तथा रूढ़िगत विचारों से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः उनके दृष्टिकोण में दूरदर्शिता का अभाव आ जाता है और उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है।
3. सकारात्मक राज्य के प्रतिकूल – न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली आधुनिक, सामाजिक व आर्थिक परिवेश के अनुपयुक्त है। न्यायाधीश प्रायः सम्पन्न वर्ग के होते हैं और वे निहित स्वार्थों का संरक्षण करते हैं। परिणामस्वरूप प्रगतिशील तथा लोकतन्त्रात्मक नीतियों का विरोध करते हैं, जिससे सकारात्मक राज्य का विकास नहीं हो पाता है। लॉस्की का कथन है-“न्यायाधीशों ने सदैव धन-सम्पन्न वर्ग के हितों की सुरक्षा की है। वह लॉर्ड सभा की भाँति ही सदैव धनिक वर्ग का गढ़ रहा है।”
4. असावधान तथा अनुत्तरदायी संसद – उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर संसद-सदस्यों द्वारा कड़े परिश्रम के बाद पारित विधि को नष्ट कर देता है। फलतः जनता के प्रतिनिधियों के प्रयास का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाता है। अतः कानून निर्माण के सम्बन्ध में वे सावधानी नहीं बरतते तथा वे अपने उत्तरदायित्व को अनुभव नहीं करते हैं।
5. कृत्रिम और शिथिल विधायिका – न्यायिक पुनर्विलोकन के कारण देश का योजनाबद्ध विकास नहीं हो पाता है तथा राजनीतिज्ञ अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पाते हैं, परिणामस्वरूप उनके कार्यों में कृत्रिमता एवं शिथिलता आ जाती है। वे व्यापक सुधार योजना लागू नहीं कर पाते हैं और केवल साधारण परिवर्तनों से उन्हें सन्तोष करना पड़ता है।
6. संसद तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष से शासन व्यवस्था में गतिरोध – न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जब सरकार के दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शासन ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन की उपयोगिता एवं महत्त्व
न्यायिक पुनर्विलोकन की उपयोगिता तथा महत्त्व को निम्नवत् स्पष्ट किया जा सकता है।
1. यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन की बहुत आलोचना हुई है तथापि इसकी उपयोगिता को भी कम नहीं आँका जाना चाहिए। इसी कारण आज तक इस विषय में उच्चतम न्यायालय के अधिकार सीमित नहीं किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा निजी सम्पत्ति के अधिकारों की भी सुरक्षा की है। प्रो० के० सी० ह्रीयर के अनुसार, “संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना उच्चतम न्यायालय की ही कार्य है।”
2. उच्चतम न्यायालय ने सदैव संविधान को अपनी व्याख्याओं के द्वारा प्रगतिशील बनाया है।
3. उच्चतम न्यायालय ने संघीय तथा राज्यों की सरकारों के वैधानिक विवादों का निर्णय करके उनको अपने क्षेत्राधिकार में रखा है। फाइनर के अनुसार, “यह एक सीमेण्ट है जिसने सम्पूर्ण संघीय ढाँचे को स्थिरता प्रदान की है।”
4. उच्चतम न्यायालय ने विधायिका तथा कार्यपालिका को एक-दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से रोका है। यह कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ही सम्भव हो सका। संघीय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
5. यदि उच्चतम न्यायालय पुनर्निरीक्षण का कार्य न करता, तो संविधान कभी भी सर्वोच्च कानून नहीं रह सकता था और संसद तथा राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा हजारों कानून इसके विरुद्ध बन जाते और संविधान महत्त्वहीन प्रलेख मात्र रह जाता। इसीलिए अपनी स्वस्थ एवं सुन्दर व्याख्याओं द्वारा उच्चतम न्यायालय ने संविधान की सुरक्षा की है, उसे गतिशील बनाया है और संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों को मनमानी करने से रोका है।
समीक्षा वर्तमान समय में न्यायिक पुनर्विलोकन की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। प्रारम्भ में न्यायाधीशों की प्रवृत्ति प्रतिक्रियावादी थी, परन्तु अब उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। और वे संसद के व्यवस्थापन क्षेत्र में कम-से-कम हस्तक्षेप करते हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरन्तर गति प्रदान करता रहा है।
प्रश्न 4.
जनहित याचिकाएँ (जनहित अभियोग) के अर्थ एवं महत्त्व पर प्रकाश डालिए। [2009]
या
‘जनहित याचिका’ से आप क्या समझते हैं? भारतीय न्याय-व्यवस्था में इनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। [2013, 14, 15]
उत्तर :
जनहित याचिकाएँ (जनहित अभियोग) का अर्थ
न्याय के प्रसंग में परम्परागत धारणा यह रही है कि न्यायालय से न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे स्वयं या जिसके पारिवारिक जन को कोई पीड़ा पहुँची है, किन्तु आज की परिस्थितियों में न्यायिक सक्रियतावाद के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आंग्ल विधि के उपर्युक्त नियम को परिवर्तित करते हुए यह व्यवस्था की है।
कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है, जिसको उसके कानून या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष ‘वाद’ ( मुकदमा ) ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी और कार्य-विधि सम्बन्धी नियमों की परवाह किये बिना ‘वाद’ लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अनुसार, वाद कारण’ और ‘पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब ‘वर्ग कार्यवाही’ और ‘लोकहित में कार्यवाही की व्यापक धारणा ने ले लिया है। ऐसे मामले व्यक्तिगत मामलों से भिन्न होते हैं। वैयक्तिक मामलों में ‘वादी’ और ‘प्रतिवादी’ होते हैं, जब कि जनहित संरक्षण से सम्बन्धित मामले किसी एक व्यक्ति के बजाय ऐसे समूह के हितों की रक्षा पर बल देते हैं जो कि शोषण और अत्याचार का शिकार होता है और जिसे संवैधानिक और मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया है। इस प्रकार के मुकदमे के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, वह जनहित याचिका’ है तथा इस प्रकार का मुकदमा जनहित अभियोग है।
जनहित याचिकाओं का महत्त्व
जनहित याचिकाओं का महत्त्व निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है –
1. समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त होना – भारत में करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो राजव्यवस्था और समाज के धनी-मानी व्यक्तियों के अत्याचार भुगत रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, लेकिन उनके पास न्यायालय में जाने के लिए आवश्यक जानकारी, समझ और साधन नहीं हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से अब समाज के शिक्षित और साधन सम्पन्न व्यक्ति इन कमजोर वर्गों की ओर से न्यायालय में जाकर इनके लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जनहित याचिकाओं की विशेष बात यह है कि ‘वाद’ प्रस्तुत करने के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं होता और इन मुकदमों में न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए आवश्यकतानुसार नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी करता है।
2. कानूनी न्याय के साथ-साथ आर्थिक-सामाजिक न्याय पर बल – जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के अन्तर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित जनों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः इन न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक-सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के हरिजनों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं उनकी आर्थिक-सामाजिक दशाओं को जाँचने के लिए एक आयोग गठित किया। आयोग की जाँच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हरिजनों का धन्धा ठेके पर दिये जाने से उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में इस बात का प्रतिपादन किया कि यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है तो वे इसे संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन और बेगार मानेंगे। इस प्रकार ‘बन्धुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार’ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बन्धुआ मुक्ति मोर्चा’ संस्था के पत्र को रिट मानकर आयोग नियुक्त कर जाँच करवाई और जाँच में जब पाया कि ‘मजदूर अमानवीय दशा में कार्यरत हैं तब न्यायालय ने इन मजदूरों की मुक्ति के आदेश दिये।
3. शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण – जनहित याचिकाओं का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण है। संविधान और कानून के अन्तर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ- ‘स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। इस पृष्ठभूमि में जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विवेकात्मक शक्तियों के अन्तर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनायी जाए, वह कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।
4. शासन को आवश्यक निर्देश देना – 1993-2003 के वर्षों में तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली। इन न्यायालयों ने जब यह देखा कि जाँच एजेन्सियाँ उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कार्य में ढिलाई बरत रही हैं तब न्यायालयों ने विभिन्न जाँच एजेन्सियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिये और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है तथा सरकारी एजेन्सी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। पिछले 20 वर्षों में जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायालयों ने बन्धुआ मजदूरी और बाल श्रम की स्थितियाँ समाप्त करने, कानून और व्यवस्था बनाये रखते हुए निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने, प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी संविधान के प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू करने, बस दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से व्यवस्था करने, सफाई की व्यवस्था कर महामारियों की रोकथाम करने, सरसों के तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और पर्यावरण की रक्षा आदि के प्रसंग में समय-समय पर अनेक आदेश-निर्देश जारी किये हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) [4 अंक]
प्रश्न 1.
लोक अदालत से आप क्या समझते हैं? भारतीय न्याय व्यवस्था में इसकी भूमिका एवं महत्त्व की चर्चा कीजिए। [2014]
उत्तर :
लोक अदालत
भारत जैसे देश में जहाँ 125 करोड़ की आबादी निवास करती है वहीं न्यायालयों के समक्ष वादों की संख्या भी अत्यधिक है। एक अध्ययन के अनुसार केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तीन लाख वादं लम्बित हैं और देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के समान होता है, अनेक ऐसे वाद हैं, जिनमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों का देहान्त हो चुका होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने लोक अदालतों की व्यवस्था आरम्भ की तथा भारत में प्रथम लोक अदालत 1982 ई० में गुजरात में आयोजित की गई।
उत्तर प्रदेश में पहली लोक अदालत का आयोजन 1984 ई० में हुआ। भारत में अधिकांश आबादी इस स्तर पर है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल से कर पाते हैं। अतः यह आबादी इन लम्बे मुकदमों को लड़ने में असमर्थ है। अतः इस सामान्य जनता के समय एवं धन की बचत के साथ-साथ न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से भी लोक अदालत की अवधारणा अमल में लाई गई।
न्याय व्यवस्था में लोक अदालतों की प्रमुख भूमिका एवं महत्त्व
लोक अदालतों की प्रमुख भूमिका एवं महत्त्व निम्नलिखित हैं –
- लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं रख सकते हैं तथा आपस में समझौता करते हैं, जिससे दोनों पक्षों के सरकारी धन की बचत होती है।
- लोक अदालतों में मुकदमों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होता है, जिससे आपसी सद्भाव एवं समरसता भी दोनों पक्षों में बनी रहती है।
- लोक अदालत में दोनों पक्षों को सलाह एवं परामर्श देने के लिए राज़पत्रित अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जिससे न केवल निर्णय की निष्पक्षता बनी रहती है, वरन् मुकदमों को सामाजिक व्यापकता भी प्रदान होती है।
- लोक अदालतों में सामाजिक एवं पारिवारिक विवाद, किराया, बेदखली बीमा, ब्याज आदि विभिन्न छोटे-छोटे मुकदमों को समझा-बुझाकर समझौता करा दिया जाता है तथा एक दिन में ही अनेकों मामले हल हो जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है एवं त्वरित न्याय प्राप्ति की व्यवस्था होती है।
- लोक अदालतों ने न केवल सामाजिक समस्याओं का हल निकाला है, वरन् अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को भी कम करने में सहायता की है।
नि:सन्देह लोक अदालतों ने सराहनीय कार्य किये हैं। विगत 33 वर्षों में इन अदालतों ने लाखों मुकदमों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाकर निपटारा किया है।
प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार क्या है? उसका एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर :
संविधान के अनुच्छेद 143 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से दो प्रकार के मामलों में अपनी राय अभिव्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। यह सलाहकारी हैसियत में होगा, न्यायिक हैसियत में नहीं।
(क) पहले वर्ग में यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि कोई विधि का प्रश्न ऐसी प्रकृति का है। और ऐसे सार्वजनिक महत्त्व का है कि जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस विधिक प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश में दी गयी राय सरकार पर आबद्धकर नहीं है, अर्थात् उसको मानने को सरकार बाध्य नहीं है। यह राय केवल सलाहकारी है। ऐसा प्रायः तभी होता है। जब सरकार कोई कार्यवाही करने से पहले प्राधिकृत विधिक राय पाने को आतुर हो। 1995 ई० तक राष्ट्रपति द्वारा इस वर्ग के 9 निर्देश किये गये हैं। अन्तिम बार 1991 ई० में ‘कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया गया था।
उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि अनुच्छेद 143 के अधीन उससे पूछा गया प्रश्न व्यर्थ या अनावश्यक है तो वह उसका उत्तर देने से मना कर दे। राष्ट्रपति ने जनवरी, 1993 ई० में सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर परामर्श माँगा था कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद से पूर्व वहाँ कोई मन्दिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 1994 को अपने सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में राय देने से मना कर दिया था।
(ख) दूसरे वर्ग के मामले में संविधान के प्रारम्भ से पहले की गयी सन्धियों और करारों से उपजे विवाद आते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विवादों की विषय-वस्तु को उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी हैसियत से राय देने के लिए भेज सकता है।

प्रश्न 3.
‘न्यायिक पुनरावलोकन’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2013]
या
न्यायिक समीक्षा के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2007]
या
न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? [2007, 10]
या
न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। [2014, 15]
उत्तर :
भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से गृहीत है। संविधानवाद को अमेरिकी संविधान निर्माताओं की कई मौलिक देन हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह सौंपा गया है कि वह विधायिका तथा कार्यपालिका को नियन्त्रित करे। चूँकि अमेरिका में संविधान सर्वोपरि है, इसलिए वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय यह देखे कि वे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस अधिकार के अन्तर्गत यदि किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कोई कानून संघीय संविधान अथवा संयुक्त राज्य द्वारा की गयी सन्धि के प्रतिकूल हो तथा कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रतिकूल हों तो संघीय न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन’ कहते हैं। कारविन के शब्दों में, “न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध व व्यर्थ समझे।’
प्रश्न 4.
न्यायिक अभिलेख (रिट) क्या है? संक्षेप में बताइए। [2016]
या
अधिकार पृच्छा का लेख से आप क्या समझते हैं? [2016]
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय संविधान की धारा-32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो आदेश जारी करता है, उसे न्यायिक अभिलेख (रिट) कहते हैं। रिट पाँच प्रकार की होती है जोकि निम्नलिखित हैं
1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण – कार्यपालिका व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार जोकि अवैध निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निरोध उचित है अथवा अनुचित है।
2. परमादेश – इसका शाब्दिक अर्थ है, ‘हम आदेश देते है। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है।
3. उत्प्रेषण – इसका शाब्दिक अर्थ है और अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।
4. अधिकार पृच्छा – जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय इस रिट द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता है।
5. प्रतिषेध – यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्धन्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें प्राधिकरण न्यायालय को – कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है।
प्रश्न 5.
भारतीय न्याय व्यवस्था में लोक अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2014]
या
लोक अदालतों के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। [2009]
या
भारतीय न्याय प्रणाली में लोक अदालतों की प्रासंगिकता के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2015]
उत्तर :
लोक अदालतें
भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था ऐसी है कि न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय और धन व्यय होता है। वर्तमान समय में न्यायालयों में लाखों की संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं। इस समस्या का समाधान करने और न्याय को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। ये अदालतें देश के विभिन्न भागों में शिविर में रूप में लगाई जा रही हैं, जहाँ पर न्यायाधीश छोटे-मोटे मुकदमों की सुनवाई करके तत्काल निर्णय दे देते हैं। इन अदालतों की प्रमुख विशेषताएँ (गुण) निम्नलिखित हैं –
- इन अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राजपत्रित अधिकारी तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में बैठते हैं।
- इन अदालतों में वादी तथा प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते हैं, बल्कि न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्ष स्वयं अपना पक्ष एवं बचाव पक्ष प्रस्तुत करते हैं।
- इन अदालतों में मुकदमों का निपटारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया जाता है।
- इन अदालतों में वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, किराया, बेदखली, वाहनों का चालान तथा बीमा आदि के मामले आते हैं।
- ये अदालतें समझौता कराती हैं, जुर्माना कर सकती हैं अथवा चेतावनी दे सकती हैं। इन अदालतों को कारावास सम्बन्धी दण्ड देने का अधिकार नहीं है।
- इन अदालतों को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिल पायी है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)
प्रश्न 1.
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में किन अर्हताओं का होना आवश्यक है?
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है।
1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है।
या वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है।
या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता है।
प्रश्न 2.
उच्चतम न्यायालय के चार प्रमुख कार्य बताइए। [2008]
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय के चार प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं –
- मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित विवादों पर उच्चतम न्यायालय फैसला देता है।
- (क) केन्द्र व राज्यों के बीच झगड़े
- (ख) राज्यों के आपसी झगड़े
- (ग) अन्तर्राज्यीय जल स्रोतों के झगड़े।
- उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों का पुनरावलोकन करता है।
- सलाहकार क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक महत्त्व के मामले में राष्ट्रपति के माँगने पर उन्हें कानूनी सलाह उपलब्ध कराता है।
- यह न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है तथा उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने में निरीक्षक की भूमिका अदा करता है।
प्रश्न 3.
“सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक ही नहीं बल्कि उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है।” इस कथन की पुष्टि कीजिए। [2007]
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय संविधान की पवित्रता की रक्षा भी करता है। यदि संसद संविधान को अतिक्रमण करके कोई कानून बनाती हैं तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, जो संविधान के विपरीत हो। इसी प्रकार वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के संविधान का अतिक्रमण करने वाले आदेशों को भी अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने वाला (Interpreter) अन्तिम न्यायालय है। संक्षेप में, कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का अधिकार है, क्योंकि इसे कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका ने सम्पत्ति के अधिकार का अतिक्रमण करने वाले अनेक कानूनों को गोलकनाथ केस, सज्जनसिंह केस तथा केशवानन्द भारती केस में अवैध घोषित किया है।
प्रश्न 4.
भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वतन्त्रता के कोई दो निर्णायक कारक बताइए। [2012]
उत्तर :
भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वतन्त्रता के दो निर्णायक कारक निम्नवत् हैं –
1. न्यायाधीशों की नियुक्ति – संविधान के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है जो मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 1998 के निर्णय के आधार पर व्यवस्था कर दी है कि अब इस प्रसंग में सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ स्थिति कहा जा सकता है।
2. दीर्घ कार्यकाल और पद की सुरक्षा – भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतया पदच्युत नहीं किया जा सकता। है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। पदच्युति की इस पद्धति को व्यवहार में अपनाया जाना बहुत कठिन होता है।
प्रश्न 5.
अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? [2013]
उत्तर :
अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं–प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किये जायेंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमान’ (Contempt of Court) के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।
प्रश्न 6
जनहित याचिकाओं के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2016]
उत्तर :
जनहित याचिकाओं के पक्ष में दो तर्क निम्नलिखित हैं –
- सरल, सस्ता, शीघ्र न्याय – जनहित याचिका द्वारा सामान्य जनता को सरल, कम व्यय में तथा जल्दी न्याय की प्राप्ति हो जाती है। अधिकांश जनहित याचिकाओं में यह देखने को मिलता है कि इसमें पीड़ित पक्ष को पर्याप्त राहत मिलती है, चूंकि जनहित याचिका को न्यायिक प्रक्रिया के जटिल विनियमों से गुजरना नहीं पड़ता है, इसमें यदि न्यायालय याचिका को निर्णय के लिए स्वीकार कर लेता है, तो उस पर कार्यवाही तुरन्त हो जाती है।
- शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक – न्यायालय ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय देकर कार्यपालिका के ढुलमुल रवैये तथा निरंकुशता पर रोक लगाई है तो उन्हें अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने का मार्ग दिखाया है।
प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल एवं उन पर महाभियोग के बारे में बताइए।
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु की समाप्ति पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यदि कोई न्यायाधीश चाहे तो इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग-पत्र देकर अपने पद-भार से मुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रमाणित दुर्व्यवहार की स्थिति में संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है।
प्रश्न 8
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? [2013]
उत्तर :
अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसके दो अर्थ हैं –
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और अदालती कार्यवाही को अभिलेख के रूप में रखा जायेगा जो अधीनस्थ न्यायालयों में दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे और उनकी प्रामाणिकता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जायेगा।
- इस न्यायालय द्वारा ‘न्यायालय की अवमानना’ के लिए दण्ड दिया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में स्वत: ही मान्य हो जाती है, लेकिन संविधान में इस न्यायालय की अवमानना करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था विशिष्ट रूप से की गयी है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न [1 अंक]
प्रश्न 1.
सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं ?
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीस अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 31 न्यायाधीश होते हैं।

प्रश्न 2
सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो कार्य अथवा अधिकार बताइए। [2010]
उत्तर :
- मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा
- संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना।
प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रमुख क्षेत्राधिकारों के वाद लिखिए। [2013, 14]
उत्तर :
- उच्चतम न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड को अपने यहाँ मँगो सकता है तथा फैसला दे सकता है।
- सरकार के ऐसे कार्यों को जो संविधान की मूल भावना के अनुकूल न हों उनका स्वयं संज्ञान लेते हुए संवैधानिक घोषित कर उनको शून्य करार दे सकता है।
प्रश्न 4.
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? [2008, 12, 14, 16]
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता क्रम के आधार पर करता है।
प्रश्न 5.
उच्चतम न्यायालय के किसी एक आरम्भिक अधिकार का उल्लेख कीजिए। [2010]
उत्तर :
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद उच्चतम न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।
प्रश्न 6.
जनहित याचिकाएँ किन न्यायालयों में दायर की जा सकती हैं? [2009]
उत्तर :
जनहित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय या जिस प्रान्त से सम्बन्धित याचिका है उस प्रान्त के उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है।
प्रश्न 7
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संविधान में क्या आधार बताये गये हैं?
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संविधान में कदाचार (प्रमाणित दुर्व्यवहार) अथवा असमर्थता (अक्षमता) को आधार बनाया गया है।
प्रश्न 8
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम-से कम कितनी अवधि के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करना आवश्यक है?
उत्तर :
कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए।
प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है?
उत्तर :
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित जो विवाद हैं, वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
प्रश्न 10
भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? [2013, 16]
उत्तर :
भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है।
प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? [2013]
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है।
प्रश्न 12.
राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन-सा है?
उत्तर :
राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है।
प्रश्न 13.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? [2016]
उत्तर :
भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
प्रश्न 14.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु क्या है? (2012)
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है।
प्रश्न 15.
भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक क्यों कहा गया है? (2008, 10, 12, 14, 15)
उत्तर :
संविधान के खिलाफ किए गए विधायिका के कार्यों का उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। तथा नागरिकों के मूल अधिकारों को बहाल करा सकने के कारण उसे संविधान व मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है।
प्रश्न 16.
लोक अदालत किसे कहते हैं?
उत्तर :
लोक अदालत में परम्परागते कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है तथा इसमें वकीलों की भी कोई भूमिका नहीं होती है। समझौते द्वारा समस्या को हल कर न्याय को सुलभ कराया जाता है।
प्रश्न 17.
जनहित मुकदमे से क्या आशय है?
उत्तर :
पददलित सामान्यजनों के हितार्थ जो मुकदमे चलाए जाते हैं, उन्हें जनहित मुकदमे कहा जाता है।

प्रश्न 18.
लोक अदालत के दो महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्लेख कीजिए।
या
लोक अदालत के दो कार्य लिखिए।
उत्तर :
- शीघ्र न्याय तथा
- कानूनी जटिलताओं से छुटकारा।
प्रश्न 19.
सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्व के पक्ष में दो तर्क दीजिए।
उत्तर :
- संविधान को संरक्षक तथा
- मूल अधिकारों का अभिरक्षक।
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? [2008, 12, 14]
(क) संसद
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) राष्ट्रपति
(घ) मन्त्रिपरिषद्
प्रश्न 2.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? [2009]
(क) इलाहाबाद में
(ख) नयी दिल्ली में
(ग) मुम्बई में
(घ) चेन्नई में
प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर कार्यरत रहता है – [2008, 10, 11, 12]
या
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की आयु है [2008, 09, 11, 12, 16]
(क) 58 वर्ष की आयु तक
(ख) 60 वर्ष की आयु तक
(ग) 65 वर्ष की आयु तक
(घ) 62 वर्ष की आयु तक
प्रश्न 4.
भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? [2013, 15, 16]
(क) राष्ट्रपति
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) सर्वोच्च न्यायालय
(घ) संसद
प्रश्न 5.
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? [2009]
(क) 23
(ख) 24
(ग) 30
(घ) 26
प्रश्न 6.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है?
(क) केन्द्रीय विधि मन्त्री
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) महान्यायवादी।
(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
प्रश्न 7.
संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों की अधिकृत भाषा है- [2012]
(क) केवल अंग्रेजी
(ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी
(ग) अंग्रेजी तथा कोई भी क्षेत्रीय भाषा
(घ) अंग्रेजी तथा आठवीं सूची में निर्दिष्ट भाषा
प्रश्न 8.
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त लिया गया है [2013, 15]
(क) फ्रांस के संविधान से
(ख) जर्मनी के संविधान से
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
(घ) कनाडा के संविधान से
प्रश्न 9.
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?
(क) अनुच्छेद 29
(ख) अनुच्छेद 31
(ग) अनुच्छेद 33
(घ) इनमें से कोई नहीं
प्रश्न 10.
उच्च न्यायालय से परामर्श माँगने का अधिकार किसको है?
(क) प्रधानमन्त्री को
(ख) लोकसभा अध्यक्ष को
(ग) राष्ट्रपति को
(घ) विधिमन्त्री को।
प्रश्न 11.
उच्च न्यायालय के वह कौन-से मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ?
(क) गजेन्द्र गडकर
(ख) एम० हिदायतुल्लाह
(ग) के० सुब्बाराव
(घ) पी० एन० भगवती
प्रश्न 12.
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है?
(क) केन्द्रीय विधि मन्त्री
(ख) प्रधानमन्त्री
(ग) महान्यायवादी
(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
प्रश्न 13.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? [2016]
(क) 65 वर्ष
(ख) 60 वर्ष
(ग) 58 वर्ष
(घ) 62 वर्ष
प्रश्न 14.
सर्वोच्च न्यायालय के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है? [2016]
(क) संसद द्वारा
(ख) राष्ट्रपति द्वारा
(ग) मंत्रिमंडल द्वारा
(घ) प्रधानमंत्री द्वारा
उत्तर :
- (ग) राष्ट्रपति
- (ख) नयी दिल्ली में
- (ग) 65 वर्ष की आयु तक
- (ग) सर्वोच्च न्यायालय
- (ग) 30
- (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (क) केवल अंग्रेजी
- (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
- (घ) इनमें से कोई नहीं
- (ग) राष्ट्रपति को
- (ख) एम० हिदायतुल्लाह
- (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश
- (घ) 62 वर्ष
- (क) संसद द्वारा।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 17 Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat (भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 17 Indian Judiciary: Supreme Court Public Interest Litigations and Lok Adalat (भारतीय न्यायपालिका-सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएँ तथा लोक अदालत), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.