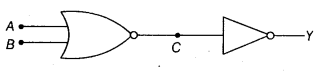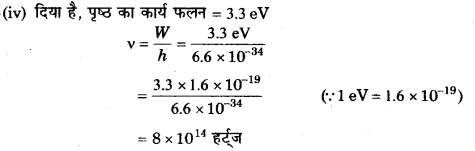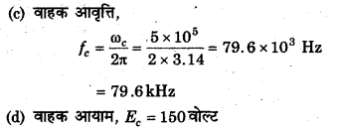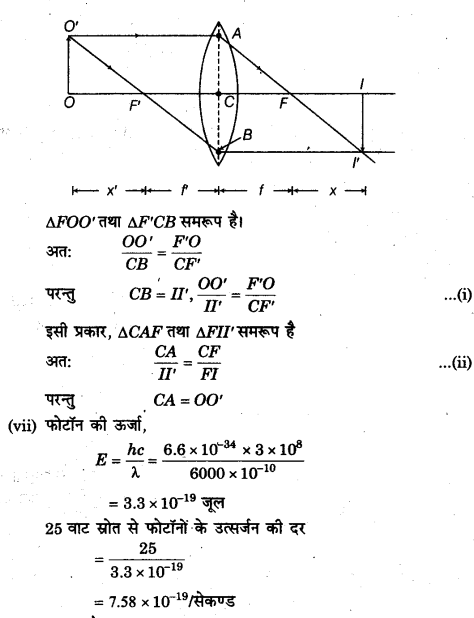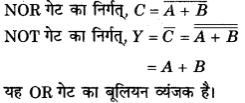UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध are part of UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध.
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Samanya Hindi |
| Chapter Name | विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध
विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध
विज्ञान : वरदान या अभिशाप [2009, 10]
सम्बद्ध शीर्षक
- विज्ञान और समाज [2011]
- विज्ञान के बढ़ते चरण
- विज्ञान के चमत्कार [2014]
- विज्ञान लाभ एवं हानि
- विज्ञान की देन
- वैज्ञानिक प्रगति और मानव-जीवन
- विज्ञान का कल्याणकारी स्वरूप
- विज्ञान का रचनात्मक स्वरूप [2013, 18]
- विज्ञान और मानव-कल्याण [2016]
प्रमुख विचार-विन्द
- प्रस्तावना,
- विज्ञान : वरदान के रूप में—(क) यातायात के क्षेत्र में; (ख) संचार के क्षेत्र में; (ग) दैनन्दिन जीवन में; (घ) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में; (ङ) औद्योगिक क्षेत्र में; (च) कृषि के क्षेत्र में; (छ) शिक्षा के क्षेत्र में; (ज) मनोरंजन के क्षेत्र में,
- विज्ञान : अभिशाप के रूप में,
- उपसंहार
प्रस्तावना-आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रान्ति ला दी है। मानव-समाज की सारी गतिविधियाँ आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्यविधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊँचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयाँ तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान-शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, किन्तु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियन्त्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित होगा।
विज्ञान : वरदान के रूप में आधुनिक मानव का सम्पूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रिया-कलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टी०वी०, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है-
आज की दुनिया विचित्र नवीन,
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन ।
हैं बँधे नर के करों में वारि-विद्युत भाप,
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप ।
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान,
लाँघ सकता नर सरित-गिरि-सिन्धु एक समान ॥
विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है-
(क) यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्य को लम्बी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किन्तु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर-से-दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुँचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गयी है। मानव केवल धरती ही नहीं, अपितु चन्द्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच गया है। अकाल, बाढ़, सूखी आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है।
(ख) संचार के क्षेत्र में-बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष (टेलीफोन, मोबाइल फोन), दूरमुद्रक (टेलीप्रिण्टर, फैक्स) आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिखाया है।
(ग) दैनन्दिन जीवन में विद्युत् के आविष्कार ने मनुष्य की दैनन्दिन सुख-सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी-सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है।
(घ) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय (टी० बी०), हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही सम्भव हुआ है। एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड टेस्ट, ऐन्जियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अन्दर के रोगों का पता सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। भीषण रोगों के लिए आविष्कृत टीकों से इन रोगों की रोकथाम सम्भव हुई है। प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण आदि उपायों से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलायी जा रही है। यही नहीं, इससे नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना सम्भव हो सका है।
(ङ) औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े-बड़े कल-कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन सम्भव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करायी जा सकी हैं।
(च) कृषि के क्षेत्र में लगभग 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है, तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादे, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे-बड़े बाँधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही सम्भव हुआ है।
(छ) शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण-यन्त्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन सम्भव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ आदि भी मुद्रण-क्षेत्र में हुई क्रान्ति के फलस्वरूप घर-घर पहुँचकर लोगों का ज्ञानवर्द्धन कर रही हैं। आकाशवाणी-दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कम्प्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है।
(ज) मनोरंजन के क्षेत्र में-चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेपरिकॉर्डर, वी० सी० आर०, वी० सी० डी० आदि ने इस दिशा में क्रान्ति ला दी है और मनुष्य को उच्चकोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव-जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है।
विज्ञान : अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव-कल्याण से कार्य किया करता है, परन्तु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्वयुद्ध का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है, जब कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम-बम गिराया गया था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानवमात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्वयुद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है; अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी है।
विध्वंसक साधनों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से भी विज्ञान ने मानव का अहित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक होता है। इस दृष्टिकोण के विकसित हो जाने के परिणामस्वरूप मानव हृदय की कोमल भावनाओं एवं अटूट आस्थाओं को ठेस पहुंची है। विज्ञान ने भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है, जिसके परिणामस्वरूप धर्म एवं अध्यात्म से सम्बन्धित विश्वास थोथे प्रतीत होने लगे हैं। मानव-जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध भी कमजोर होने लगे हैं। अब मानव भौतिक लाभ के आधार पर ही सामाजिक सम्बन्धों को विकसित करता है।
जहाँ एक ओर विज्ञान ने मानव-जीवन को अनेक प्रकार की सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव-जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कम्प्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराये हैं तो साथ-साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिये हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान् देन है, परन्तु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की इहलीला समाप्त कर सकता है। विज्ञान ने तरह-तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिये हैं। इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गॅवा देते हैं। विज्ञान के दिन-प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असन्तुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है।
अधिक सुख-सुविधाओं के कारण मनुष्य आलसी और आरामतलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और अनेक नये-नये रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। मानव में सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गयी है।
वाहनों की बढ़ती संख्या से सड़कें पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो रही हैं तो उनसे निकलने वाले ध्वनि प्रदूषक मनुष्य को स्नायु रोग वितरित कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएँ तो मानो दिनचर्या का एक अंग हो चली हैं। विज्ञापनों ने प्राकृतिक सौन्दर्य को कुचल डाला है। चारों ओर का कृत्रिम आडम्बरयुक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण-प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं।
विज्ञान के इसी विनाशकारी रूप को दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं—
सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार।
तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार ॥
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार।
काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार ॥
उपसंहार–विज्ञान सचमुच तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकती है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख-समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणु-शक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित सम्भावनाओं का द्वार उन्मुक्त कर सकता है। बड़े-बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लंघ्य पर्वतों पर मार्ग बनाकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल बाँधों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में इसका उपयोग हो सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव-कल्याण की सात्त्विक भावना जगे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे।
धर्म और विज्ञान [2016]
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- धर्म और विज्ञान का विरोध,
- धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू,
- धर्म मनुष्य को भीरु बनाता है और विज्ञान साहसी,
- धर्म भी विज्ञान है और विज्ञान भी धर्म है,
- उपसंहार
प्रस्तावना-संस्कृत में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है–‘ध्रियते लोकोऽनेन, धरति लोकं वा।’ अर्थात् इस संसार के धारण करने योग्य जो भी बातें हैं, वे सभी धर्म हैं और वे सभी बातें धारण करने योग्य हैं, जो संसार के लिए कल्याणकारी हैं। विज्ञान भी उन्हीं सब कार्यों अथवा अनुसन्धानों को करने की अनुमति प्रदान करता है, जो संसार के लिए कल्याणकारी हैं। इस प्रकार धर्म और विज्ञान का उद्देश्य एक ही है।
धर्म और विज्ञान का विरोध-आध्यात्मिक स्तर पर धर्म और विज्ञान दो विपरीत विचारधाराएँ हैं। धर्म परम-सुख (मोक्ष/परमानन्द) की प्राप्ति के लिए भौतिकवाद का विरोध करते हुए उसे त्यागने की बात करता है, जबकि विज्ञान भौतिक संसार से बाहर किसी सुख की सत्ता तो स्वीकार नहीं करता; अतः वह मनुष्य को परम-सुख की प्राप्ति के लिए भौतिकवाद में किण्ठ डूबने के लिए प्रेरित करता है।
धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू-वस्तुत: धर्म और विज्ञान दो विरोधी अवधारणाएँ नहीं हैं, वरन् एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही सत्य के रूप का उद्घाटन करते हैं। हाँ, सत्य के उद्घाटन की दोनों की पद्धतियाँ अवश्य ही अलग-अलग हैं। जहाँ एक ओर धर्म ने मानव को मानसिक शान्ति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान ने भौतिक सुख। धर्म ने मानव के हृदय को परिष्कृत किया है तो विज्ञान ने उसकी बुद्धि को।
धर्म मनुष्य को भीरु बनाता है और विज्ञान साहसी-धर्म सर्वशक्तिमान् एवं अनादि ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय और भीरु बनाता है। इसी भीरुता के कारण मनुष्य ईश्वर की आलोचना करने से डरता है। ईश्वर के प्रति उसकी अटूट आस्था एवं विश्वास उसे भाग्यवादी बनाकर अकर्मण्य बनाते हैं, जबकि विज्ञान मनुष्य को निर्भीक और साहसी बनाकर उसे निरन्तर कर्म करते हुए रहने की प्रेरणा प्रदान करता है।
धर्म भी विज्ञान है और विज्ञान भी धर्म है-धर्म और विज्ञान का जो विरोध दृष्टिगत होता है, वह धर्म से सम्बन्धित पाखण्डों, अन्धविश्वासों, अन्धश्रद्धा और कर्मकाण्डों की अधिकता और अनिवार्यता के कारण है। वस्तुतः धर्म को यदि हम उसकी परिभाषा के आलोक में देखें तो पाते हैं कि धर्म किसी भी अतार्किक बात की स्वीकृति नहीं देता, वह विज्ञान की भाँति ठोस तर्को का पक्षपाती है। वह भी एक विज्ञान है, जो तर्कों के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके उसे तर्कपूर्ण विधियों से प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।
धार्मिक लोग जिस भौतिकवाद की दुहाई देकर विज्ञान की आलोचना करते हैं, वह वास्तव में उनका अज्ञान है। विज्ञान केवल मनुष्य के कल्याण का पक्षपाती है, उसने अग्नि की खोज खाना पकाने और ऊर्जा के स्रोत के रूप में मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए की, अब अगर कोई उसकी अग्नि से किसी का घर जलाने लगे तो उसमें विज्ञान का क्या दोष? विज्ञान ने तो अपना धर्म निभाते हुए मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए अग्नि की खोज की, अब अगर अधर्म का आचरण करके मनुष्य किसी का घर जलाकर विनाश को आमन्त्रण दे तो इससे विज्ञान की धार्मिकता कहाँ कम होती है। धर्म वही है, जिसे प्राणिमात्र के कल्याण केलिए धारण किया जाए तो विज्ञान भी वही है, जिसका प्रत्येक अनुसन्धान प्राणिमात्र के कल्याण के लिए है। इस प्रकार विज्ञान ही धर्म है।।
उपसंहार-आज यदि आवश्यकता है तो विज्ञान एवं धर्म के पारस्परिक समन्वय की है, क्योंकि न तो विज्ञान से विमुख धर्म मनुष्य का कल्याण करने में समर्थ है और न ही विज्ञान धर्म से अलग होकर अपने कल्याणकारी स्वरूप की रक्षा कर सकता है।
कम्प्यूटर : आधुनिक मानव-यन्त्र [2013, 15, 16]
सम्बद्ध शीर्षक
- कम्प्यूटर के प्रयोग से लाभ तथा हानि [2013]
- कम्प्यूटर की उपयोगिता [2010]
- कम्प्यूटर का महत्त्व
- कम्प्यूटर की आत्मकथा
- भारत में कम्प्यूटर का महत्त्व [2013, 14, 18]
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना : कम्प्यूटर क्या है ?
- कम्प्यूटर के उपयोग,
- कम्प्यूटर तकनीक से हानियाँ,
- कम्यूटर और मानव-मस्तिष्क,
- उपसंहार
प्रस्तावना--कम्प्यूटर असीमित क्षमताओं वाला वर्तमान युग का एक क्रान्तिकारी साधन है। यह एक ऐसा यन्त्र-पुरुष है, जिसमें यान्त्रिक मस्तिष्कों को रूपात्मक और समन्वयात्मक योग तथा गुणात्मक घनत्व पाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप यह कम-से-कम समय में तीव्रगति से त्रुटिहीन गणनाएँ कर लेता है। आरम्भ में, गणित की जटिल गणनाएँ करने के लिए ही कम्प्यूटर का आविष्कार किया गया था। आधुनिक कम्प्यूटर के प्रथम सिद्धान्तकार चार्ल्स बैबेज ( सन् 1792-1871 ई०) ने गणित और खगोल-विज्ञान की सूक्ष्म सारणियाँ तैयार करने के लिए ही एक भव्य कम्प्यूटर की योजना तैयार की थी। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में अमेरिकी इंजीनियर हरमन होलेरिथ ने जनगणना से सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए पंचका पर आधारित कम्प्यूटर का प्रयोग किया था। दूसरे महायुद्ध के दौरान पहली बार बिजली से चलने वाले कम्प्यूटर बने। इनका उपयोग भी गणनाओं के लिए ही हुआ। आज के कम्प्यूटर केवल गणनाएँ करने तक ही सीमित नहीं रह गये हैं वरन् अक्षरों, शब्दों, आकृतियों और कथनों को ग्रहण करने में अथवा इससे भी अधिक अनेकानेक कार्य करने में समर्थ हैं। आज कम्प्यूटरों का मानव-जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों में उपयोग करना सम्भव हुआ है। अब कम्प्यूटर संचार और नियन्त्रण के भी शक्तिशाली साधन बन गये हैं।
कम्प्यूटर के उपयोग-आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों के व्यापक उपयोग हो रहे हैं—
(क) प्रकाशन के क्षेत्र में सन् 1971 ई० में माइक्रोप्रॉसेसर का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने कम्प्यूटरों को छोटा, सस्ता और कई गुना शक्तिशाली बना दिया। माइक्रोप्रॉसेसर के आविष्कार के बाद कम्प्यूटर का अनेक कार्यों में उपयोग सम्भव हुआ। शब्द-संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) कम्प्यूटरों के साथ स्क्रीन व प्रिण्टर जुड़ जाने से इनकी उपयोगिता का खूब विस्तार हुआ है। सर्वप्रथम एक लेख सम्पादित होकर कम्प्यूटर में संचित होता है। टंकित मैटर को कम्प्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद मशीनों से छपाई होती है। अब तो अतिविकसित देशों (ब्रिटेन आदि) में बड़े समाचार-पत्रों में सम्पादकीय विभाग में एक सिरे पर कम्प्यूटरों में मैटर भरा जाता है तथा दूसरे सिरे पर तेज रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक प्रिण्टर समाचार-पत्र छापकर निकाल देते हैं।
(ख) बैंकों में कम्प्यूटर का उपयोग बैंकों में किया जाने लगा है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुम्बकीय संख्याओं वाली चेक-बुक भी जारी कर दी हैं। खातों के संचालन और लेन-देन का हिसाब रखने वाले कम्प्यूटर भी बैंकों में स्थापित हो रहे हैं। आज कम्प्यूटर के द्वारा ही बैंकों में 24 घण्टे पैसों के लेन-देन की ए० टी० एम० (Automated Teller Machine) जैसी सेवाएँ सम्भव हो सकी हैं। यूरोप और अमेरिका में ही नहीं अब भारत में भी ऐसी व्यवस्थाएँ अस्तित्व में आ गयी हैं कि घर के निजी कम्प्यूटरों के जरिये बैंकों से भी लेन-देन का व्यवहार सम्भव हुआ है।
(ग) सूचनाओं के आदान-प्रदान में प्रारम्भ में कम्प्यूटर की गतिविधियाँ वातानुकूलित कक्षों तक ही सीमित थीं, किन्तु अब एक कम्प्यूटर हजारों किलोमीटर दूर के दूसरे कम्प्यूटरों के साथ बातचीत कर सकता है तथा उसे सूचनाएँ भेज सकता है। दो कम्प्यूटरों के बीच यह सम्बन्ध तारों, माइक्रोवेव तथा उपग्रहों के जरिये स्थापित होता है। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए देश के सभी प्रमुख छोटे-बड़े शहरों को कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिये एक-दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। इण्टरनेट जैसी सुविधा से आज देश का प्रत्येक नगर सम्पूर्ण विश्व से जुड़ गया है।
(घ) आरक्षण के क्षेत्र में कम्प्यूटर नेटवर्क की अनेक व्यवस्थाएँ अब हमारे देश में स्थापित हो गयी हैं। सभी प्रमुख एयरलाइन्स की हवाई यात्राओं के आरक्षण के लिए अब ऐसी व्यवस्था है कि भारत के किसी शहर से आपकी समूची हवाई यात्रा के आरक्षण के साथ-साथ विदेशों में आपकी इच्छानुसार होटल भी आरक्षित हो जाएगा। कम्प्यूटर नेटवर्क से अब देश के सभी प्रमुख शहरों में रेल-यात्रा के आरक्षण की व्यवस्था भी अस्तित्व में आ गयी है।
(ङ) कम्प्यूटर ग्राफिक्स में कम्प्यूटर केवल अंकों और अक्षरों को ही नहीं, वरन् रेखाओं और आकृतियों को भी सँभाल सकते हैं। कम्प्यूटर ग्राफिक्स की इस व्यवस्था के अनेक उपयोग हैं। भवनों, मोटरगाड़ियों, हवाई-जहाजों आदि के डिज़ाइन तैयार करने में कम्प्यूटर ग्राफिक्स का व्यापक उपयोग हो रहा है। वास्तुशिल्पी अब अपने डिज़ाइन कम्प्यूटर स्क्रीन पर तैयार करते हैं और संलग्न प्रिण्टर से इनके प्रिण्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि कम्प्यूटर चिप्स के सर्किटों के डिजाइन भी अब कम्प्यूटर ग्राफिक्स की मदद से तैयार होने लगे हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान भी कम्प्यूटर के स्क्रीन पर किये जा रहे हैं।
(च) कला के क्षेत्र में कम्प्यूटर अब चित्रकार की भूमिका भी निभाने लगे हैं। चित्र तैयार करने के लिए अब रंगों, तूलिकाओं, रंग-पट्टिका और कैनवास की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। चित्रकार अब कम्प्यूटर के सामने बैठता है और अपने नियोजित प्रोग्राम की मदद से अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रीन पर रंगीन रेखाएँ प्रस्तुत कर देता है। रेखांकनों से स्क्रीन पर निर्मित कोई भी चित्र ‘प्रिण्ट’ की कुञ्जी दबाते ही, अपने समूचे रंगों के साथ कम्प्यूटर से संलग्न प्रिण्टर द्वारा कागज पर छाप दिया जाता है।
(छ) संगीत के क्षेत्र में कम्प्यूटर अब सुर सजाने का काम भी करने लगे हैं। पाश्चात्य संगीत के स्वरांकन को कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु वीणा जैसे भारतीय वाद्य की स्वरलिपि तैयार करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, परन्तु वह दिन दूर नहीं है जब भारतीय संगीत की स्वर-लहरियों को कम्प्यूटर स्क्रीन पर उभारकर उनका विश्लेषण किया जाएगा और संगीत-शिक्षा की नयी तकनीक विकसित की जा सकेंगी।
(ज) खगोल-विज्ञान के क्षेत्र में कम्प्यूटरों ने वैज्ञानिक अनुसन्धान के अनेक क्षेत्रों का समूचा ढाँचा ही बदल दिया है। पहले खगोलविद् दूरबीनों पर रात-रातभर आँखें गड़ाकर आकाश के पिण्डों का अवलोकन करते थे, किन्तु अब किरणों की मात्रा के अनुसार ठीक-ठीक चित्र उतारने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हो गये हैं। इन चित्रों में निहित जानकारी का व्यापक विश्लेषण अब कम्प्यूटरों से होता है।
(झ) चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी एक सरल कम्प्यूटर ही है। मतदान के लिए ऐसी वोटिंग मशीनों का उपयोग सीमित पैमाने पर ही सही अब हमारे देश में भी हो रहा है।
(ज) उद्योग-धन्धों में कम्प्यूटर उद्योग-नियन्त्रण के भी शक्तिशाली साधन हैं। बड़े-बड़े कारखानों के संचालन का काम अब कम्प्यूटर सँभालने लगे हैं। कम्प्यूटरों से जुड़कर रोबोट अनेक किस्म के औद्योगिक उत्पादनों को सँभाल सकते हैं। कम्प्यूटर भयंकर गर्मी और ठिठुरती सर्दी में भी यथावत् कार्य करते हैं। इनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे देश में अब अधिकांश निजी व्यवसायों में कम्प्यूटर का प्रयोग होने लगा है।
(ट) सैनिक कार्यों में आज प्रमुख रूप से महायुद्ध की तैयारी के लिए नये-नये शक्तिशाली सुपर कम्प्यूटरों का विकास किया जा रहा है। हाशक्तियों की ‘स्टार वार्स’ की योजना कम्प्यूटरों के नियन्त्रण पर आधारित है। पहले भारी कीमत देकर हमारे देश में सुपर कम्प्यूटर आयात किये जा रहे थे; परन्तु अब इन सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण हमारे देश में भी किया जा रहा है।
(ठ) अपराध निवारण में अपराधों के निवारण में भी कम्प्यूटर की अत्यधिक उपयोगिता है। पश्चिम के कई देशों में सभी अधिकृत वाहन मालिकों, चालकों, अपराधियों का रिकॉर्ड पुलिस के एक विशाल कम्प्यूटर में संरक्षित होता है। कम्प्यूटर द्वारा क्षण मात्र में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जो कि अपराधियों के पकड़ने में सहायक सिद्ध होती है। यही नहीं, किसी भी अपराध से सन्दर्भित अनेकानेक तथ्यों में से विश्लेषण द्वारा कम्प्यूटर नये तथ्य ढूंढ़ लेता है तथा किसी अपराधी को कैसा भी चित्र उपलब्ध होने पर वह उसकी सहायता से अपराधी के किसी भी उम्र और स्वरूप की तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है।
कम्प्यूटर तकनीक से हानियाँ-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर तकनीकी के निरन्तर बढ़ते जा रहे व्यापक उपयोगों ने जहाँ एक ओर इसकी उपयोगिता दर्शायी है, वहीं दूसरी ओर इसके भयावह परिणामों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कम्प्यूटर हर क्षेत्र में मानव-श्रम को नगण्य बना देगा, जिससे भारत सदृश जनसंख्या बहुल देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। विभिन्न विभागों में इसकी स्थापना से कर्मचारी भविष्य के प्रति अनाश्वस्त हो गये हैं।
बैंकों आदि में इस व्यवस्था के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आये हैं। दूसरों के खातों के कोड नम्बर जानकर प्रति वर्ष करोड़ों डॉलरों से बैंकों को ठगना अमेरिका में एक आम बात हो गयी है। हमारे देश के बैंकों में बिना कम्प्यूटरों के करोड़ों की ठगी के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी इसके परिणाम शत-प्रतिशत सही नहीं निकले हैं।
कम्प्यूटर और मानव-मस्तिष्क-कम्प्यूटर के सन्दर्भ में ढेर सारी भ्रान्तियाँ जनसामान्य के मस्तिष्क में छायी हुई हैं। कुछ लोग इसे सुपर पावर समझ बैठे हैं, जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है। किन्तु उनकी धारणाएँ पूर्णरूपेण निराधार हैं। वास्तविकता तो यह है कि कम्प्यूटर एकत्रित आँकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली एक मशीन मात्र है। यह केवल वही काम कर सकता है, जिसके लिए इसे निर्देशित किया गया हो। यह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। यह मानवीय संवेदनाओं, अभिरुचियों, भावनाओं और चित्त से रहित मात्र एक यन्त्र-पुरुष है, जिसकी बुद्धि-लब्धि (Intelligence Quotient : I.O.) मात्र एक मक्खी के बराबर होती है, यानि बुद्धिमत्ता में कम्प्यूटर मनुष्य से कई हजार गुना पीछे है।।
उपसंहार-निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी के भी दो पक्ष हैं। इसको सोच समझकर उपयोग किया जाए तो यह वरदान सिद्ध हो सकता है, अन्यथा यह मानव-जाति की तबाही का साधन भी बन सकता है। इसीलिए कम्प्यूटर की क्षमताओं को ठीक से समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा एवं साधन; कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी की उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इनके लिए यदि बुनियादी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती, देश में टेक्नोलॉजी के साधन जुटाये जाते और पाश्चात्य संस्कृति में विकसित हुई इस टेक्नोलॉजी को देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धीरे-धीरे अपनाया जाता तो अच्छा होता।।
इण्टरनेट
सम्बद्ध शीर्षक
- इण्टरनेट : लाभ और हानियाँ [2017, 18]
- भारत में इण्टरनेट का विकास
- सूचना प्रौद्योगिकी और मानव-कल्याण [2013, 14]
- इण्टरनेट की शैक्षिक उपयोगिता [2016]
प्रमुखविचार-बिन्दु–
- भूमिका,
- इतिहास और विकास,
- इण्टरनेट सम्पर्क,
- इण्टरनेट सेवाएँ,
- भारत में इण्टरनेट,
- भविष्य की दिशाएँ,
- उपसंहार
भूमिका-इण्टरनेट ने विश्व में जैसा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, वैसा किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी ने नहीं किया। नेट के नाम से लोकप्रिय इण्टरनेट अपने उपभोक्ताओं के लिए बहुआयामी साधन प्रणाली है। यह दूर बैठे उपभोक्ताओं के मध्य अन्तर-संवाद का माध्यम है; सूचना या जानकारी में भागीदारी और सामूहिक रूप से काम करने का तरीका है; सूचना को विश्व स्तर पर प्रकाशित करने का जरिया है और सूचनाओं को अपार सागर है। इसके माध्यम से इधर-उधर फैली तमाम सूचनाएँ प्रसंस्करण के बाद ज्ञान में परिवर्तित हो रही हैं। इसने विश्व-नागरिकों के बहुत ही सुघड़ और घनिष्ठ समुदाय का विकास किया है।
इण्टरनेट विभिन्न टेक्नोलॉजियों के संयुक्त रूप से कार्य का उपयुक्त उदाहरण है। कम्प्यूटरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम्प्यूटर सम्पर्क-जाल का विकास, दूर-संचार सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता और घटता खर्च तथा आँकड़ों के भण्डारण और सम्प्रेषण में आयी नवीनता ने नेट के कल्पनातीत विकास और उपयोगिता को बहुमुखी प्रगति प्रदान की है। आज किसी समाज के लिए इण्टरनेट वैसी ही ढाँचागत आवश्यकता है जैसे कि सड़कें, टेलीफोन या विद्युत् ऊर्जा।
इतिहास और विकास–इण्टरनेट का इतिहास पेचीदा है। इसका पहला दृष्टान्त सन् 1962 ई० में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान के जे० सी० आर० लिकप्लाइडर द्वारा लिखे गये कई ज्ञापनों के रूप में सामने आया था। उन्होंने कम्प्यूटर की ऐसी विश्वव्यापी अन्तर्सम्बन्धित श्रृंखला की कल्पना की थी जिसके जरिये वर्तमान इण्टरनेट की तरह ही आँकड़ों और कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार के नेटवर्क में सहायक बनी तकनीकी सफलता पहली बार इसी संस्थान के लियोनार्ड क्लिनरोक ने सुझायी थी। उनकी यह सूझ पैकेट स्विचिंग नाम की नयी टेक्नोलॉजी थी जो सामान्य टेलीफोन प्रणाली में प्रयुक्त सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी से मिलती-जुलती थी। पैकेट स्विचिंग उस पत्र पेटी की तरह थी, जिसका इस्तेमाल चाहे जितने लोग कर सकते थे। इसके जरिये दुनिया में कम्प्यूटर अन्य कम्प्यूटरों से जुड़े बिना भी एक-दूसरे से संवाद कायम कर सकते थे।
इण्टरनेट के इतिहास में 1973 का वर्ष ऐसा था जिसने अनेक मील के पत्थर जोड़े और इस प्रकार अधिक विश्वसनीय और स्वतन्त्र नेटवर्क की शुरुआत हुई। इसी वर्ष में इण्टरनेट ऐक्टिविटीज बोर्ड की स्थापना की गयी। इस वर्ष के नवम्बर महीने में डोमेन नेमिंग सर्विस (डीएनएस) का पहला विवरण जारी किया गया और वर्ष की आखिरी महत्त्वपूर्ण घटना इण्टरनेट का सेना और आम लोगों के लिए उपयोग के वर्गीकरण द्वारा सार्वजनिक नेटवर्क के उदय के रूप में सामने आया तथा इसी के साथ आज प्रचलित इण्टरनेट ने जन्म लिया।
इण्टरनेट का बाद का इतिहास मुख्यत: बहुविध उपयोग का है जो नेटवर्क की आधारभूत संरचना से ही सम्भव हो सका। बहुविध उपयोग की दिशा में पहला कदम फाइल ट्रांसफर प्रणाली का विकास था। इससे दूर-दराज के कम्प्यूटरों के बीच फाइलों का आदान-प्रदान सम्भव हो सका। सन् 1984 ई० में इण्टरनेट से जुड़े कम्प्यूटरों की संख्या 1000 थी जो सन् 1989 ई० में एक लाख के ऊपर पहुँच चुकी थी। 90 के दशक के आरम्भ में इण्टरनेट पर सूचना प्रस्तुति के नये तरीके सामने आये। सन् 1991 ई० में मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार गोफर नामक सरलता से पहुँच योग्य डाक्युमेण्ट प्रस्तुति प्रणाली अस्तित्व में आयी। इससे पहले सन् 1990 ई० में ही टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब (www) का आविष्कार करके सूचना प्रस्तुति का एक नया तरीका सामने रखा जो सरलता से इस्तेमाल योग्य सिद्ध हुआ।
सन् 1993 ई० में ट्रैफिकल वेब ब्राउजर का आविष्कार इण्टरनेट के क्षेत्र में एक बड़ी घटना थी। इससे न केवल विवरण वरन चित्रों का भी दिग्दर्शन सम्भव हो गया। इस वेब ब्राउजर को मोजाइक कहा गया। इस समय तक इण्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 20 लाख से अधिक हो गयी थी और आज प्रचलित इण्टरनेट आकार ले चुका था।
इण्टरनेट सम्पर्क–इण्टरनेट का आधार राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सूचना इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है जो सामान्यत: हाइबैण्ड विड्थ ट्रंक लाइनों से बना होता है और जहाँ से विभिन्न सम्पर्क लाइनें कम्प्यूटरों को जोड़ती हैं जिन्हें आश्रयदाता (होस्ट) कम्प्यूटर कहते हैं। ये आश्रयदाता कम्प्यूटर प्रायः बड़े संस्थानों; जैसे—विश्वविद्यालयों, बड़े उद्यमों और इण्टरनेट कम्पनियों से जुड़े होते हैं और इन्हें इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) कहा जाता है। आश्रयदाता कम्प्यूटर चौबीसों घण्टे काम करते हैं और अपने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं। ये कम्प्यूटर विशेष संचार लाइनों के जरिये इण्टरनेट से जुड़े रहते हैं। इनके उपभोक्ताओं/व्यक्तियों के पीसी (पर्सनल कम्प्यूटर) साधारण टेलीफोन लाइन और मोडेम के जरिए इण्टरनेट से जुड़े रहते हैं।
एक सामान्य उपभोक्ता एक निश्चित राशि का भुगतान करके आईएसपी से अपना इण्टरनेट खाता प्राप्त कर लेता है। आईएसपी लॉगइन नेम, पासवर्ड (जिसे उपभोक्ता बदल भी सकता है) और नेट से जुड़ने के लिए कुछ एक जानकारियाँ उपलब्ध करा देता है। एक बार इण्टरनेट से जुड़ जाने पर उपभोक्ता इण्टरनेट की तमाम सेवाओं तक अपनी पहुँच बना सकता है। इसके लिए उसे सही कार्यक्रम का चयन करना होता है। ज्यादातर इण्टरनेट सेवाएँ उपभोक्ता-सर्वर रूपाकार पर काम करती हैं। इनमें सर्वर वे कम्प्यूटर हैं जो नेट से जुड़े हुए व्यक्तिगत कम्प्यूटर उपभोक्ताओं को एक या अधिक सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। इसे सेवा के वास्तविक प्रयोग के लिए उपभोक्ता को उस विशेष सेवा के लिए आश्रित (क्लाइण्ट) सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है।
इण्टरनेट सेवाएँ-इण्टरनेट की उपयोगिता उपभोक्ता को उपलब्ध सेवाओं से निर्धारित होती है। इसके उपभोक्ता को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध हैं-
(क) ई-मेल-ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इण्टरनेट का सबसे लोकप्रिय उपयोग है। संवाद के अन्य माध्यमों की तुलना में सस्ता, तेज और अधिक सुविधाजनक होने के कारण इसने दुनिया भर के घरों और कार्यालयों में अपनी जगह बना ली है। इसके द्वारा पहले भाषायी पाठ ही प्रेषित किया जा सकता था, लेकिन अब सन्देश, चित्र, अनुकृति, ध्वनि, आँकड़े आदि भी प्रेषित किये जा सकते हैं।
(ख) टेलनेट-टेलनेट एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता को किसी दूर स्थित कम्प्यूटर से स्वयं को जोड़ने की सुविधा प्राप्त हो जाती है।
(ग) इण्टरनेट चर्चा (चैट)–नयी पीढ़ी में इण्टरनेट रिले चैट या चर्चा व्यापक रूप से लोकप्रिय है। यह ऐसी गतिविधि है, जिसमें भौगोलिक रूप से दूर स्थित व्यक्ति एक ही चैट सर्वर पर लॉग करके की-बोर्ड के जरिये एक-दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए एक वांछित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो निश्चित समय पर उस लाइन पर सुविधापूर्वक उपलब्ध हो।।
(घ) वर्ल्ड वाइड वेब–यह सुविधा इण्टरनेट के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित उपयोगों में से एक है। यह इतनी आसान है कि इसके प्रयोग में बच्चों को भी कठिनाई नहीं होती। यह मनचाही संख्या वाले अन्तर्सम्बन्धित डॉक्युमेण्ट का समूह है, जिसमें से प्रत्येक डॉक्युमेण्ट की पहचान उसके विशेष पते से की जा सकती है। इस पर उपलब्ध सबसे महत्त्वपूर्ण सेवाओं में से एक सर्विंग है। इण्टरनेट में शताधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं जिनमें गूगल सर्वाधिक लोकप्रिय है।
(ङ) ई-कॉमर्स-इण्टरनेट की प्रगति की ही एक परिणति ई-कॉमर्स है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय को संचालित करने के लिए इण्टरनेट पर की जाने वाली कार्यवाही को ई-कॉमर्स कहते हैं। इसके अन्तर्गत वस्तुओं का क्रय-विक्रय, विभिन्न व्यक्तियों या कम्पनियों के मध्य सेवा या सूचना आते हैं।
इन मुख्य सेवाओं के अतिरिक्त इण्टरनेट द्वारा और भी अनेक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिनके असीमित उपयोग हैं।
भारत में इण्टरनेट–भारत में इण्टरनेट का आरम्भ आठवें दशक के अन्तिम वर्षों में अनेट (शिक्षा और अनुसन्धान नेटवर्क) के रूप में हुआ था। इसके लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी थी। इस परियोजना में पाँच प्रमुख संस्थान, पाँचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक निदेशालय शामिल थे। अनेंट का आज व्यापक प्रसार हो चुका है और वह शिक्षा और शोध समुदाय को देशव्यापी सेवा दे रहा है। एक अन्य प्रमुख नेटवर्क नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेण्टर (एनआईसी) के रूप में सामने आया, जिसने प्राय: सभी जनपद मुख्यालयों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ दिया। आज देश के विभिन्न भागों में यह 1400 से भी अधिक स्थलों को अपने नेटवर्क के जरिये जोड़े हुए है।
आम आदमी के लिए भारत में इण्टरनेट का आगमन सन् 15 अगस्त, 1995 ई० को हो गया था, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने देश में अपनी सेवाओं का आरम्भ किया। प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक इण्टरनेट की पहुँच काफी धीमी रही, लेकिन हाल के वर्षों में इसके उपभोक्ता की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सन् 1999 ई० में टेलीकॉम क्षेत्र निजी कम्पनियों के लिए खोल दिये जाने के परिणामस्वरूप अनेक नये सेवा प्रदाता बेहद प्रतिस्पर्धा विकल्पों के साथ सामने आये। भारत में इण्टरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष अप्रैल 2010 तक 7 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। भारत में इण्टरनेट का उपयोग करने वाले विश्व की तुलना में 5% हैं और भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। सरकारी एजेंसियाँ इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि आईटी का लाभ सामान्य जन तक पहुँचाया जा सके। भारतीय रेल द्वारा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा शहरों के मध्य सूचना प्रणाली की स्थापना तथा केरल सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फास्ट रिलायबिल इन्स्टेण्ट एफीशिएण्ट नेटवर्क फॉर डिस्बर्समेण्ट ऑफ सर्विसेज (फ्रेण्ड्स) जैसी पेशकशों ने इस दिशा में देश के आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है।
भविष्य की दिशाएँ-भविष्य के प्रति इण्टरनेट बहुत ही आश्वस्तकारी दिखाई दे रहा है और आज के आधार पर कहीं अधिक प्रगतिशाली सेवाएँ प्रदान करने वाला होगा। भविष्य के नेटवर्क जिन उपकरणों और साधनों को जोड़ेगे, वे मात्र कम्प्यूटर नहीं होंगे, वरन् माईक्रोचिप से संचालित होने के कारण तकनीकी अर्थों में कम्प्यूटर जैसे होंगे। आने वाले समय में केवल कार्यालय ही नहीं निवास, स्कूल, अस्पताल और हवाई अड्डे एक-दूसरे से जुड़े हुए होंगे। व्यक्ति के पास व्यक्तिगत डिजीटल सहायक ऐसे पाम टॉप होंगे, जो वायरलेस और मोबाइल टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके किसी भी उपलब्ध नेटवर्क से स्वतः जुड़ जाएँगे। लोग अपने मोबाइल फोन के जरिये ही विभिन्न देयों का भुगतान कर सकेंगे और कारें हाईवे पर भीड़-भाड़ पर नजर रखने और अपने चालकों को सुविधाजनक रास्ते के बारे में सुझाव देने में समर्थ होंगी। इण्टरनेट व्यक्तियों और समुदायों को परस्पर घनिष्ठ रूप से काम के लिए सक्षम बना देगा और भौगोलिक दूरी के कारण आने वाली बाधाओं को समाप्त कर देगा। कम्प्यूटर रचित समुदायों का उदय हो जाएगा और तब दमनकारी शासकों के लिए विश्व में अपनी लोकप्रियता को सुरक्षित रख पाना सम्भव नहीं रह जाएगा। भविष्य में टेक्नोलॉजी का उपयोग संस्कृति, भाषा और विरासत की विविधता की रक्षा के लिए किया जाएगा तथा भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी।
उपसंहार-टेक्नोलॉजियों के लोकप्रिय होते ही सामान्य शिक्षित नागरिकों के लिए भी यह पूरी तरह आसान हो जाएगा कि वह कानून-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकें। इसके फलस्वरूप कहीं अधिक समर्थ लोकतन्त्र सम्भव हो सकेगा जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व कुछ अलग प्रकार के होंगे। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती इण्टरनेट टेक्नोलॉजी के दोहन की है जिससे समाज के हर वर्ग तक उसके फायदों की पहुँच सम्भव बनायी जा सके। किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमेशा समूचे समाज के लिए होना चाहिए न कि उसको समाज के कुछ वर्गों को वंचित करने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार यह उपलब्धि हासिल की जा सके तो वास्तव में सम्भावनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। संक्षेप में, क्रान्ति तो अभी आरम्भ ही हुई है।
भारत की वैज्ञानिक प्रगति
सम्बद्ध शीर्षक
- भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ
- भारतीय विज्ञान की देन
प्रमुख विचार-बिन्द–
- प्रस्तावना,
- स्वतन्त्रता पूर्व और पश्चात् की स्थिति,
- विभिन्न क्षेत्रों में हुई वैज्ञानिक प्रगति,
- उपसंहार
प्रस्तावना—सामान्य मनुष्य की मान्यता है कि सृष्टि का रचयिता सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो इस संसार का निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वह ईश्वर के प्रतिरूप ब्रह्मा (निर्माता), विष्णु (पालनकर्ता) और महेश (संहारकर्ता) को चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से परखनली शिशु उत्पन्न करके उसने ब्रह्मा की सत्ता को ललकारा है, बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना कर और लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार देकर उसने विष्णु को चुनौती दी है तथा सर्व-विनाश के लिए परमाणु बम का निर्माण कर उसने शिव को चकित कर दिया है।
विज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय में विशेष ज्ञान विज्ञान मानव के लिए कामधेनु की तरह है जो उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है तथा उसकी कल्पनाओं को साकार रूप देता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान प्रवेश कर चुका है चाहे वह कला का क्षेत्र हो या संगीत और राजनीति का। विज्ञान ने समस्त पृथ्वी और अन्तरिक्ष को विष्णु के वामनावतार की भाँति तीन डगों में नाप डाला है।।
स्वतन्त्रता पूर्व और पश्चात् की स्थिति–बीसवीं शताब्दी को विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ हासिल करने के कारण विज्ञान का युग कहा गया है। आज संसार ने ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति कर ली है। भारत भी इस क्षेत्र में किसी अन्य वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों से यदि आगे नहीं, तो बहुत पीछे या कम भी नहीं है। 15 अगस्त, सन् 1947 में जब अंग्रेजों की गुलामी का जूआ उतार कर भारत स्वतन्त्र हुआ था, तब तक कहा जा सकता है कि भारत वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर शून्य से अधिक कुछ भी नहीं था। सूई तक का आयात इंग्लैण्ड आदि देशों से करना पड़ता था। लेकिन आज सुई से लेकर हवाई जहाज, जलयान, सुपर कम्प्यूटर, उपग्रह तक अपनी तकनीक और बहुत कुछ अपने साधनों से इस देश में ही बनने लगे हैं। लगभग पाँच दशकों में इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास करके भारत ने केवल विकासोन्मुख राष्ट्रों को ही नहीं, वरन् उन्नत एवं विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों को भी चकित कर दिया है। भारतीय प्रतिभा का लोहा आज सम्पूर्ण विश्व मानने लगा है।
विभिन्न क्षेत्रों में हुई वैज्ञानिक प्रगति–डाक-तार के उपकरण, तरह-तरह के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडियो-टेलीविजन, कारें, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, रेलवे इंजिन और यात्री तथा अन्य प्रकार के डिब्बे, कल-कारखानों में काम आने वाली छोटी-बड़ी मशीनें, कार्यालयों में काम आने वाले सभी प्रकार के सामान, रबर-प्लास्टिक के सभी प्रकार के उन्नत उपकरण, कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट तथा अन्य कटाई-धुनाई–पिसाई की मशीनें आदि सभी प्रकार के आधुनिक विज्ञान की देन माने जाने वाले साधन आज भारत में ही बनने लगे हैं। कम्प्यूटर, छपाई की नवीनतम तकनीक की मशीनें आदि भी आज भारत बनाने लगा है। इतना ही नहीं, आज भारत में अणु शक्ति से चालित धमन भट्टियाँ, बिजली घर, कल-कारखाने आदि भी चलने लगे हैं तथा अणु-शक्ति का उपयोग अनेक शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए होने लगा है। पोखरण में भूमिगत अणु-विस्फोट करने की बात तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है।
आज भारतीय वैज्ञानिक अपने उपग्रह तक अन्तरिक्ष में उड़ाने तथा कक्षा में स्थापित करने में सफल हो चुके हैं। आवश्यकता होने पर संघातक अणु, कोबॉल्ट और हाइड्रोजन जैसे बम बनाने की दक्षता भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हासिल कर ली है। विज्ञान-साधित उपकरणों, शस्त्रास्त्रों का आज सैनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व बढ़ गया है। अपने घर बैठकर शत्रु देश के दूर-दराज के इलाकों पर आक्रमण कर पाने की वैज्ञानिक विधियाँ और शस्त्रास्त्र आज विशेष महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। धरती से धरती तक, धरती से आकाश तक मार कर सकने वाली कई तरह की मिसाइलें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनायी गयी हैं जो आज भारतीय सेना के पास हैं और अन्य अनेक का विकास-कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। युद्धक टैंक, विमान, दूर-दूर तक मार करने वाली तोपें आदि भारत में ही बन रही हैं। कहा जा सकता है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की सहायता से विश्व के सैन्य अभियान जिस दिशा में चल रहे हैं, भारत भी उस दिशा में किसी से पीछे नहीं है। गणतन्त्र दिवस की परेड के अवसर पर प्रदर्शित उपकरणों से यह स्पष्ट हो जाता है। फिर भी भारत को इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है।
विज्ञान ने भारतीयों के रहन-सहन और चिन्तन-शक्ति को पूर्णरूपेण बदल डाला है। भारत हवाई जहाज, समुद्र के वक्षस्थल को चीरने वाले जहाज, आकाश का सीना चीर कर निकल जाने वाले रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह आदि के निर्माण में अपना अग्रणी स्थान रखता है। 19 अप्रैल, 1975 को सोवियत प्रक्षेपण केन्द्र से ‘आर्यभट्ट’ नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर भारत ने अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया और तब से आज तक उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। स्क्वैडून लीडर राकेश शर्मा 1984 ई० में रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ अन्तरिक्ष यात्रा भी कर चुके हैं। भास्कर, ऐपल, इन्सेट, रोहिणी जैसे अनेक उपग्रह अन्तरिक्ष में स्थापित कर भारत विश्व की महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा है। इन उपग्रहों से हमें मौसम सम्बन्धी जानकारी मिलती है तथा संचार व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है।
आधुनिक विज्ञान की सहायता से आज भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। एक्सरे, लेसर किरणें आदि की सहायता से अब भारत में ही असाध्य समझे जाने वाले अनेक रोगों के उपचार होने लगे हैं। हृदय-प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, जैसे कठिन-से-कठिन माने जाने वाले ऑपरेशन आज भारतीय शल्य-चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक सम्पादित किये जा रहे हैं। सभी प्रकार की बहुमूल्य प्राण-रक्षक ओषधियों का निर्माण भी यहाँ होने लगा है।
ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति सराहनीय है। इन्होंने नदियों की मदमस्त चाल को बाँधकर उनके जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत निर्माण में किया। सौर ऊर्जा, पवन चक्कियाँ, ताप बिजलीघर, परमाणु बिजलीघर आदि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति को दर्शाते हैं। महानगरों में गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण, सड़कें, फ्लाईओवर, सब-वे आदि हमारी अभियान्त्रिकीय प्रगति को दर्शाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भीतर से जल, अनेक खनिज और समुद्र को चीर कर तेल के कुएँ भी खोज निकाले हैं। बॉम्बे हाई से तेल को उत्खनन इसका जीता-जागता उदाहरण है।
कुछ एक अपवादों को छोड़कर, भारत में अधिकांश कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से हो सकने सम्भव हो गये हैं। मानव का कार्य अब इतना ही रह गया है कि वह इन मशीनों पर नियन्त्रण रखे। आटा पीसने से लेकर गूंधने तक, फसल बोने से लेकर अनाज को बोरियों में भरने, वृक्ष काटने से लेकर फर्नीचर बनाने तक सभी कार्य भारत में निर्मित मशीनों द्वारा सम्पन्न होने लगे हैं। विज्ञान ने मानव के दैनिक जीवन के लिए भी अनेक क्रान्तिकारी सुविधाएँ जुटायी हैं। रेडियो, फैक्स, रंगीन टेलीविजन, टेपरिकॉर्डर, वी० सी० आर०, सी० डी० प्लेयर, दूरभाष, कपड़े धोने की मशीन, धूल-मिट्टी हटाने की मशीन, कूलर, पंखा, फ्रिज, एयरकण्डीशनर, हीटर आदि आरामदायक मशीनें भारत में ही बनने लगी हैं, जिनके अभाव में मानव-जीवन नीरस प्रतीत होता है। घरों में लकड़ी-कोयले से जलने वाली अँगीठी का स्थान कुकिंग गैस ने और गाँवों में उपलों से जलने वाले चूल्हों का स्थान गोबर गैस संयन्त्र ने ले लिया है। चलचित्रों के क्षेत्र में हमारी प्रगति सराहनीय है। कम्प्यूटर का प्रवेश और उसका विस्तार हमारी तकनीकी प्रगति की ओर इंगित करते हैं।
उपसंहार-घर-बाहर, दफ्तर-दुकान, शिक्षा-व्यवसाय, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ विज्ञान का प्रवेश न हुआ हो। भारत का होनहार वैज्ञानिक हर दिशा, स्थल और क्षेत्र में सक्रिय रहकर अपनी निर्माण एवं नव-नव अनुसन्धान प्रतिभा का परिचय दे रहा है। इतना ही नहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने विदेशों में भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा की धूम मचा रखी है। आज भारत में जो कृषि या हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आदि सम्भव हो पायी है, उन सबका कारण विज्ञान और उसके द्वारा प्रदत्त नये-नये उपकरण तथा ढंग ही हैं। आज हम जो कुछ भी खाते-पीते और पहनते हैं, सभी के पीछे किसी-न-किसी रूप में विज्ञान को कार्यरत पाते हैं। विज्ञान को कार्यरत करने वाले कोई विदेशी नहीं, वरन् भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। उन्हीं की लगन, परिश्रम और कार्य-साधना से हमारा देश भारत आज इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर सका है। भविष्य में यह और भी अधिक, सारे संसार से बढ़कर वैज्ञानिक प्रगति कर पाएगा इस बात में कतई कोई सन्देह नहीं।
मनोरंजन के आधुनिक साधन
सम्बद्ध शीर्षक
- मनोरंजन के विविध प्रकार
प्रमुख विचार-बिन्दु–
- प्रस्तावना : जीवन में मनोरंजन का महत्त्व,
- मनोरंजन के साधनों का विकास,
- आधुनिक काल में मनोरंजन के विविध साधन–(क) वैज्ञानिक साधन; (ख) अध्ययन; (ग) ललित कला सम्बन्धी; (घ) खेल सम्बन्धी; (ङ) विविध,
- उपसंहार
प्रस्तावना : जीवन में मनोरंजन का महत्त्व-जीवन में मनोरंजन मानो सब्जी में नमक की भाँति आवश्यक है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। यह उसे प्रसन्नचित्त बनाने की गारण्टी तथा जीवन के कटु अनुभवों को भुलाने की ओषधि दोनों ही है। एक नन्हा शिशु भी इसको आकांक्षी है और एक वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए भी यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है। बच्चों को बेवजह रोना इस बात का संकेत है कि वह उकता रहा है। यदि वृद्ध सनकी और चिड़चिड़े हो उठते हैं तो उसका कारण भी मनोरंजन का अभाव ही है।
मनोरंजन वस्तुत: हमारे जीवन की सफलता का मूल है। मनोरंजनरहित जीवन हमारे लिए भारस्वरूप बन जाएगा। यह केवल हमारे मस्तिष्क के लिए ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए भी परमावश्यक है। मनोरंजन के विविध रूप-खेलकूद, अध्ययन व सुन्दर दृश्यों के अवलोकन से हमारा हृदय असीम आनन्द से भर उठता है। इससे शरीर के रक्त-संचार को नवीन गति और स्फूर्ति मिलती है तथा हमारे स्वास्थ्य की अभिवृद्धि भी होती है।
मनोरंजन के साधनों का विकास मनोरंजन की इसी गौरव-गरिमा के कारण बहुत प्राचीन काल से ही मानव-समाज मनोरंजन के साधनों का उपयोग करता आया है। शिकार खेलना, रथ दौड़ाना आदि विविध कार्य प्राचीन काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे, परन्तु आजकल युग के परिवर्तन के साथ-साथ मनोरंजन के साधन भी बदल गये हैं। विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में क्रान्ति कर दी है। आज कठपुतलियों का नाचे जनसमाज की आँखों के लिए उतना प्रिय नहीं रहा, जितना कि सिनेमा के परदे पर हँसते-बोलते नयनाभिराम दृश्य।
आधुनिक काल में मनोरंजन के विविध साधन–
(क) वैज्ञानिक साधन–सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन आदि विज्ञान प्रदत्त मनोरंजन के साधनों ने आधुनिक जनसमाज में अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। साप्ताहिक अवकाश के दिनों में जनता की भारी भीड़ सिनेमाघरों की खिड़की पर दृष्टिगोचर होती है। रेडियो तो मनोरंजन का पिटारा है। इसे अपने घर में रख सुन्दर गाने, भाषण, समाचार आदि सुन सकते हैं। टेलीविजन तो इससे भी आगे बढ़ गया है। इसमें तो बोलने वाले को सशरीर अपने नेत्रों के सम्मुख देखा जा सकता है तथा विविध कार्यक्रमों, खेलों आदि के सजीव प्रसारण को देखकर पर्याप्त मनोरंजन किया जा सकता है।
(ख) अध्ययन–साहित्य का अध्ययन भी मनोरंजन की श्रेणी में आता है। यह हमें मानसिक आनन्द देता है और चित्त को प्रफुल्लित करता है। पत्र-पत्रिकाएँ और उपन्यास रेल-यात्रा के दौरान बड़े सहायक होते हैं। साहित्य द्वारा होने वाले मनोरंजन से मन की थकान ही नहीं मिटती, ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती है।
(ग) ललित-कला सम्बन्धी--संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला आदि ललित-कलाएँ भी मनोरंजन के उत्कृष्ट साधन हैं। संगीत के मधुर स्वरों में आत्म-विस्मृत करने की अपूर्व शक्ति होती है।
(घ) खेल सम्बन्धी–ललित-कलाओं के साथ-साथ खेल भी मनोरंजन के प्रिय विषय हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिण्टन आदि खेलों से खिलाड़ी एवं दर्शकों का बहुत मनोरंजन होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खेल बहुत ही हितकर हैं। इनके द्वारा उनका मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बड़े-बड़े नगरों में तो इस प्रकार के खेलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शकगण पैसा व समय खर्च करके आनन्द लूटते हैं। गर्मी की साँय-साँय करती लूओं से भरे वातावरण में घर बैठकर साँप-सीढ़ी, लूडो, ताश, कैरम, शतरंज खूब खेले जाते हैं। ये खेल प्रायः ऐसे लोगों का मनोरंजन अधिक करते हैं, जो घर से बाहर निकलना पसन्द ही नहीं करते या कम निकलते हैं।
(ङ) विविध-कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने में ही आनन्द की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लोग अपने कार्य-स्थलों से लौटने के बाद अपने उद्यान को ठीक प्रकार से सँवारने में ही घण्टों व्यतीत कर देते हैं, इससे ही इनका मनोरंजन हो जाती है। कुछ लोगों का मनोरंजन फोटोग्राफी होता है। गले में कैमरा लटकाया और चल दिये घूमने। कहीं मन-लुभावना आकर्षक-सी दृश्य दिखाई दिया और उन्होंने उसे कैमरे में कैद कर लिया। इसी से मन प्रफुल्लित हो उठा। कुछ लोगों का शौक होता है देश-विदेश की टिकटें एकत्रित करने का। इस संग्रह में ही उनका अधिकांश समय बीत जाता है। पुराने लिफाफों पर से टिकटें उतारने में ही उन्हें आनन्द आता है।
मेले-तमाशे, सैर-सपाटे, यात्रा-देशाटन आदि मनोरंजन के विविध साधन हैं। इनसे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ-ही-साथ हमारा व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। देशाटन द्वारा विविध स्थान और वस्तुएँ देखने को प्राप्त होती हैं। राहुल सांकृत्यायन तो देशाटन द्वारा अर्जित ज्ञान के कारण ही महापण्डित कहलाये और देशाटन से प्राप्त होने वाले ज्ञान और मिलने वाले मनोरंजन पर ‘घुमक्कड़-शास्त्र’ ही लिख डाला। सन्तों ने तो हर काम को हँसते-खेलते अर्थात् मनोरंजन करते हुए करने को कहा है। यहाँ तक कि ध्यान (Meditation) भी मन को प्रसन्न करते हुए किया जा सकता है—हसिबो खेलिबो धरिबो ध्यानं ।
उपसंहार निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीवन में अन्य कार्यों की भाँति मनोरंजन भी उचित मात्रा में होना ही चाहिए। सीमा से अधिक मनोरंजन समय जैसी अमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करता है। जिस प्रकार आवश्यकता से अधिक भोजन अपच का कारण बन शरीर के रुधिर-संचार में विकार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अधिक मनोरंजन भी हानिकारक होता है। हमें चाहिए कि उचित मात्रा में मनोरंजन करते हुए अपने जीवन को उल्लासमय और सरल बनायें।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.