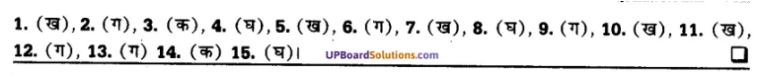UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम–कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम–कारण तथा परिणाम (अनुभाग – एक)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
1857 ई० के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। [2012]
या
1857 ई० की क्रान्ति के सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए।
या
1857 ई० के स्वतन्त्रता संघर्ष के किन्हीं तीन कारणों का वर्णन करें और इसकी असफलता के कोई दो कारण भी लिखिए। [2012]
या
1857 ई० की क्रान्ति के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। [2013]
या
अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति 1857 ई० के विद्रोह का एक प्रमुख कारण थी। स्पष्ट कीजिए।
या
भारत के लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असन्तुष्ट थे ? उनके असन्तोष के किन्हीं चार कारणों पर प्रकाश डालिए। [2015]
या
1857 ई० के भारत में क्रान्ति का स्वरूप क्या था? उसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। [2016]
उत्तर :
1857 ई० की क्रान्ति (स्वाधीनता संग्राम) का स्वरूप
निःसन्देह 1857 ई० का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व युगान्तकारी घटना है। इस क्रान्ति के स्वरूप के विषय में मुख्य रूप से दो भिन्न मत हैं। अंग्रेजों ने, जो साम्राज्यवाद के स्वाभाविक पक्षपाती थे, इसे केवल सैनिकों के (UPBoardSolutions.com) संघर्ष की संज्ञा दी है, जबकि भारतीयों ने इसे निर्विवाद रूप से प्रथम स्वाधीनता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन बताया है।
![]()
1857 ई० की क्रान्ति के विषय में कतिपय इतिहासकारों एवं विद्वानों के मत इस प्रकार हैं
सर जॉन लारेन्स के अनुसार-“यह एक सैनिक क्रान्ति थी।”
सर जेम्स आउटरम के अनुसार-“यह एक मुस्लिम षड्यन्त्र था, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से निकालकर पुन: देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने का सशस्त्र प्रयत्न किया था।”
वीर सावरकर के अनुसार-“यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था।”
अशोक मेहता के अनुसार-“यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन था।”
पी०ई० राबर्ट्स के अनुसार-“यह केवल एक सैनिक संघर्ष था, जिसका तत्कालीन कारण कारतूस वाली घटना थी। इसका किसी पूर्वगामी षड्यन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं था।”
एल०ई०आर० रीज के अनुसार-“यह धर्मान्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।”
निष्कर्षत: अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ई० का स्वतन्त्रता संग्राम भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम ही था जो सैनिक क्रान्ति के माध्यम से प्रारम्भ हुआ था। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया।
1857 ई० की क्रान्ति को भारतीय इतिहास (UPBoardSolutions.com) में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसे भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 ई० की क्रान्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। जब से अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया, भारतीय जनता में तभी से असन्तोष की लहर दौड़ रही थी। अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों ने भारतीयों में अत्यधिक असन्तोष भर दिया था और 1857 ई० की क्रान्ति उसी का परिणाम थी। 1857 ई० की क्रान्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे
(क) राजनीतिक कारण
1857 ई० की क्रान्ति के प्रमुख राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे –
1. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्वार्थपूर्ण नीति – भारत पर अपने शासन का प्रभुत्व जमाने वाली कम्पनी स्वार्थ पर आधारित थी। यह किसी भी रूप में भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं करती थी। अधिकांश अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने कम्पनी की स्वार्थ-लिप्सा को ही पूरा करने का प्रयत्न किया। कम्पनी का दोषपूर्ण शासन और अमानवीय व्यवहार इस क्रान्ति की नींव बना।
2. मुगल सम्राटों की दयनीय स्थिति – मुगल सम्राटों की स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही थी। पहले | सिक्कों पर मुगल शासकों के नाम मुद्रित किये जाते थे और कम्पनी के उच्च पदाधिकारी तक उनको झुककर सलाम करते थे, किन्तु 1835 ई० के बाद से कम्पनी ने मुगलों को बहुत ही पंगु बना दिया। सिक्कों से उनका नाम हटा दिया गया और अंग्रेज पदाधिकारियों ने उनका सम्मान करना भी छोड़ दिया।
3. उच्च नौकरियों में भारतीयों की उपेक्षा – उच्च नौकरियों में भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। लॉर्ड विलियम बैंटिंक के 1835 ई० में वापस जाने के बाद भारतीयों की पुन: उपेक्षा शुरू हो गयी थी। इस स्थिति में, भारतीयों में स्वाभाविक रूप से असन्तोष उत्पन्न हो गया।
4. दोषपूर्ण न्याय-प्रणाली – कम्पनी ने जो न्याय-प्रणाली स्थापित कर रखी थी, उससे भारतीयों को पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं होता था। यह न्याय-प्रणाली बहुत जटिल थी। इस दूषित न्याय-प्रणाली ने भारतीयों के असन्तोष में और अधिक (UPBoardSolutions.com) वृद्धि कर दी।
5. प्रशासनिक अधिकारियों का दुर्व्यवहार – ब्रिटिश प्रशासनिक व राजस्व अधिकारी जनता पर मनमाने व अमानवीय अत्याचार किया करते थे। यह दुर्व्यवहार भी क्रान्ति का एक कारण बना था।
6. लॉर्ड डलहौजी की राज्य-अपहरण की नीति – लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए सभी प्रकार की नैतिकताओं और आदर्शों को त्यागकर, उचित-अनुचित का विवेक किये बिना साम्राज्य–विस्तार की नीति को ही सर्वोपरि महत्त्व दिया। मुगल बादशाह, अवध के नवाब ‘ (वाजिद अली शाह) और मराठों को उसने अत्यधिक क्षति पहुँचायी। राज्य-अपहरण की नीति में ‘गोद निषेध नियम’ बनाकर उसने अनेक राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह राज्य-अपहरण की नीति प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का मुख्य कारण थी।
7. पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति – लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन तथा उपाधियों को भी बन्द करवा दिया। नाना साहब की पेंशन के साथ-साथ जो सम्मानसूचक उपाधि क्रमागत रूप से चली आ रही थी, समाप्त कर दी गयी। इस कारण नाना साहब स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रगण्य नेता बन गये।
![]()
(ख) आर्थिक कारण
1857 ई० की क्रान्ति के लिए निम्नलिखित आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे –
1. भारतीय व्यापार को क्षति – ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय व्यापार नष्ट हो गया। यहाँ के कच्चे माल को अंग्रेज सस्ते मूल्य पर खरीदकर इंग्लैण्ड ले जाते और उससे तैयार माल बनाकर बेचते थे। इस व्यापारिक क्षति ने भारतीय व्यापारियों और बेरोजगार हुए कारीगरों में विद्रोह की भावना जगा दी।
2. हस्तशिल्पियों की दुर्दशा – भारत का आर्थिक जनजीवन हस्तशिल्पियों पर निर्भर था। कम्पनी के व्यापार के बाद से इन हस्तशिल्पियों के दुर्दिन आ गये। इन हस्तशिल्पियों की दुर्दशा ने क्रान्ति की स्थिति में वृद्धि कर दी।
3. किसानों की दयनीय स्थिति – कम्पनी के राज्य में कृषकों की दशा दयनीय थी। भारतीय पदाधिकारी, जमींदार के ठेकेदार, कम्पनी के छोटे कर्मचारी, सभी ने कृषकों का शोषण किया। किसानों की यह विवशता एक दिन उग्र क्रान्ति का रूप बनकर ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गयी।
4. भारतीय धन का ब्रिटेन चले जाना – कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारी कुछ थोड़े समय के लिए भारत आया करते थे। अतः वे अपनी जेबें भरने के लिए लालायित रहते थे। कम्पनी भी अपनी कोष बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी। इस दोहरी मार ने साधारण भारतीयों को अपार क्षति पहुँचाई। इसीलिए भारतीय, ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए लालायित हो गये।
5. जमींदारी प्रथा के दोष – अंग्रेजों ने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया था, इससे जमींदारी प्रथा के अनेक दोष प्रकट हुए। चूँकि जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल किया करते थे, इससे किसानों को अपार कष्ट (UPBoardSolutions.com) मिलता था। जब स्वयं कुछ जमींदार लगान न देने के कारण जमींदारी से हटा दिये गये, तो वे अंग्रेजों के शत्रु बन गये। इस तरह जमींदारी से हटाये गये जमींदार एवं शोषित कृषक संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो गये।
![]()
(ग) सामाजिक कारण
1857 ई० की क्रान्ति के प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित थे –
1. सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबन्ध – सुधारों के नाम पर जिन गवर्नरों ने सामाजिक प्रथाओं (विधवा-विवाह, सती–प्रथा, बाल-विवाह) पर रोक लगायी वे यथार्थ में तो उपयोगी थे, परन्तु इससे तात्कालिक रूप से सरकार के विरुद्ध असन्तोष पैदा हुआ था।
2. पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचलन – अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का भी प्रचार किया। उन्होंने भारतीय साहित्य और प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। भारतीय जनता ने इस भाषा का विरोध किया।
3. अंग्रेजी शिक्षा का विरोध – गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक और उसके कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले के सहयोग से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाने लगी। यह शिक्षा कालान्तर में राष्ट्रीय उत्थान में सहायक सिद्ध हुई, परन्तु शुरू में इसके विरुद्ध असन्तोष पनपा
4. श्रेष्ठता की भावना – भारत में उच्च प्रशासनिक (UPBoardSolutions.com) पदों पर अंग्रेज ही आसीन थे और उनके अधीन अंग्रेजी शिक्षित भारतीय कार्य करते थे। अंग्रेज अधिकारी तो भारतीयों को निम्न श्रेणी का समझते ही थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय भी उनका पक्ष लेते हुए भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। अत: लोगों में अंग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यवहार के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न होने लगा था।
(घ) धार्मिक कारण
1857 ई० की क्रान्ति के प्रमुख धार्मिक कारण निम्नलिखित थे –
1. ईसाई धर्म का प्रचार – भारत में ईसाई पादरियों ने मिशनरियों के माध्यम से भारतीयों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर ईसाई बनाया था। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष उत्पन्न हुआ और क्रान्ति के बीज अंकुरित हुए।
2. हिन्दू और इस्लाम धर्म की अवहेलना – अंग्रेजों ने भारत के दोनों मुख्य धर्मो-हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म की अवहेलना की। वे इन धर्मों का तनिक भी आदर नहीं करते थे। यह स्थिति जनता के प्रबल असन्तोष का कारण बनी थी।
3. गोद निषेध नियम – भारतीय परम्परानुसार जो दम्पति नि:सन्तान होते थे, वे किसी दूसरे बालक को गोद ले लेते थे। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम बनाकर इस परम्परा पर कुठाराघात किया तथा अनेक राज्यों का अपहरण कर लिया।
4. ईसाइयों को विशेष सुविधाएँ – ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को सामाजिक और धार्मिक स्तर पर अनेक सुविधाएँ प्रदान की गयी थीं। नये बने ईसाई भी अनेक प्रकार की सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे। सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति ने भारतीयों में असन्तोष की वृद्धि कर दी।
5. चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग – भारतीय सैनिकों को दिये गये नये कारतूसों को राइफलों में भरने के लिए मुँह से छीलना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गयी कि इन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी मिली होती है। गाय हिन्दुओं (UPBoardSolutions.com) के लिए पवित्र थी, जबकि सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। परिणामत: हिन्दू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस क्रान्ति को ही 1857 ई० के स्वतन्त्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है।
![]()
(ङ) सैनिक कारण
1857 ई० की क्रान्ति के प्रमुख सैनिक कारण अग्रलिखित थे –
1. सैनिकों में भेदभाव – अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभाव रखा गया था। भारतीयों को वेतन, भत्ते, पदोन्नति भी कम दी जाती थी तथा इन्हें उच्च पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता था।
2. ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सैनिकों की समस्या – अंग्रेजी सेना में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। इन वर्गों के लोगों का समाज में बहुत सम्मानित स्थान था, परन्तु ब्रिटिश सेना में इनके साथ बहुत ही निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था। इस कारण भी सैनिकों के मन में असन्तोष की भावना व्याप्त थी।
3. अफगान युद्ध का प्रभाव – ब्रिटिश सैनिक 1838-42 ई० के प्रथम अफगान युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो गये थे। इससे भारतीय सैनिकों में यह धारणा व्याप्त हुई कि यदि अफगानी सैनिक ब्रिटिश सैनिकों को हरा सकते हैं, तो हम भी अपने देश को इनसे मुक्त करा सकते हैं।
4. क्रीमिया का युद्ध – यूरोप में 1854-56 ई० में हुए क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों की पर्याप्त सेना समाप्त हो गयी थी। अत: भारतीयों ने उचित अवसर पाकर क्रान्ति करने का निश्चय कर लिया था।
5. विदेश जाने की समस्या – सन् 1856 ई० में एक कानून यह बनाया गया कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए विदेश में भी भेजा जा सकता है तथा भारतीय सैनिक वहाँ जाने से मना नहीं कर सकते।
6. रियासती सेना की समाप्ति – सन् 1856 ई० में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया और वहाँ की रियासती सेना को भंग कर दिया गया। इससे साठ हजार सैनिक बेकार हो गये। इसी प्रकार ग्वालियर, मालवा आदि राज्यों की सेनाएँ भी समाप्त कर दी गयीं। (UPBoardSolutions.com) बेकार भारतीय सैनिक भड़क उठे। तथा क्रान्ति की योजनाएँ बनाने लगे।
[असफलता के कारण – इसके लिए निम्नलिखित प्रश्न संख्या 2 को उत्तर देखें।]
[परिणाम – इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखें।
![]()
प्रश्न 2.
1857 ई० की क्रान्ति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। [2009, 10, 12]
या
1857 की क्रान्ति की असफलता के प्रमुख दो कारण लिखिए। (2013)
या
1857 के स्वतन्त्रता संघर्ष की असफलता के क्या कारण थे ? किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। [2013, 17]
उत्तर :
1857 ई० की क्रान्ति की असफलता के कारण
सन् 1857 ई० की क्रान्ति या संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे –
1. समय से पूर्व क्रान्ति का प्रारम्भ – क्रान्ति के प्रारम्भ करने की तिथि 31 मई निश्चित की गयी थी, परन्तु कुछ भारतीय सैनिकों ने आवेश में आकर 10 मई को ही क्रान्ति का बिगुल बजा दिया। इस प्रकार निर्धारित समय से पूर्व क्रान्ति प्रारम्भ हो जाने के कारण संगठित क्रान्ति का प्रयास असफल हो गया और क्रान्तिकारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी।
2. क्रान्ति का सीमित क्षेत्र – इस क्रान्ति का क्षेत्र देशव्यापी न होकर सीमित था। यह क्रान्ति दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ही सीमित रही। पंजाब, राजस्थान, सिन्ध तथा पूर्वी बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का अन्त करने के लिए तनिक भी प्रयत्न नहीं किया (UPBoardSolutions.com) गया, वरन् पंजाब, राजपूताना, ग्वालियर, इन्दौर आदि, के नरेशों ने अंग्रेजों की सहायता की। सर डब्ल्यू० रसल ने लिखा है, “यदि सारे देशवासी, सर्वतोभाव से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गये होते, तो अपने साहस के रहते भी अंग्रेज पूर्णतया नष्ट कर दिये गये होते।”
3. संगठन का अभाव – क्रान्तिकारी नेताओं में संगठन का सर्वथा अभाव था। प्रत्येक की नीति अलग-अलग थी और प्रत्येक के समर्थक अपने ही नेता के नेतृत्व में काम करना चाहते थे। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है, “यदि शिवाजी या बांबर जैसा नेता होता तो वह अपने चुम्बकीय व्यक्तित्व से क्रान्ति के विभिन्न वर्गों को एक कर लेता, परन्तु ऐसे नेता के अभाव में विभिन्न लोगों के व्यक्तिगत ईष्र्या-द्वेष सामूहिक कार्य के बीच आते रहे।
4. एक लक्ष्य का अभाव – क्रान्तिकारियों का कोई एक लक्ष्य न था। वे भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब पेंशन चाहते थे, लक्ष्मीबाई गोद लेने का अधिकार और बहादुरशाह जफर बादशाहत चाहते थे।
5. कुछ भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति – क्रान्ति की विफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि कुछ भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित की। उन्होंने क्रान्तिकारियों का साथ नहीं दिया और क्रान्ति का दमन करने में अंग्रेजी सेना की सहायता की।
6. सफल नेतृत्व का अभाव – क्रान्ति के नेताओं में कोई कुशल तथा अनुभवी नेता नहीं था। बहादुरशाह तथा कुँवरसिंह वृद्ध थे। सूबेदार बख्त खाँ तथा तांत्या टोपे वीर होते हुए भी साधारण कोटि के व्यक्ति थे। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना होते हुए भी स्त्री थीं। नाना साहब में रणनीतिज्ञता का अभाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस क्रान्ति की विभिन्न शक्तियों का यथेष्ट समीकरण न हो सका। इसके विपरीत अंग्रेजों की ओर नील, हैवलॉक, आउटरम तथा यूरोज जैसे योग्य सेनापति एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे।
7. साधनों व अनुशासन का अभाव – क्रान्तिकारियों के पास साधनों का अभाव था। उनके पास धन तथा आधुनिक ढंग के अस्त्र-शस्त्रों की कमी थी। इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारियों में अनुशासन का अभाव था। वे एक (UPBoardSolutions.com) अनुशासनहीन-अनियन्त्रित क्रान्तिकारियों की भीड़ के समान थे। अनुशासन तथा सामग्री का अभाव भी इस क्रान्ति की असफलता का एक मुख्य कारण बना।
8. अंग्रेजों के पास पर्याप्त साधन – अंग्रेजों को इंग्लैण्ड से सैनिक और युद्ध-सामग्री की आपूर्ति बराबर मिलती रहती थी तथा यातायात के साधनों, रेल, तार आदि पर भी उनका अधिकार था। अतः वे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से आ-जा सकते थे तथा सन्देश भेज सकते थे। परन्तु क्रान्तिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा सन्देश भेजने में पर्याप्त समय लगता था।
9. रचनात्मक कार्यक्रमों का अभाव – क्रान्तिकारियों ने सामान्य जनता के समक्ष भविष्य का कोई रचनात्मक कार्य नहीं रखा। इस कारण सामान्य जनता का भी इन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त न हो सका।
10. वीभत्स और क्रूर अत्याचार – अंग्रेजों के वीभत्स और क्रूर अत्याचार भी क्रान्ति की असफलता के कारण बने। उनके अत्याचारों से भारतीय जनता इतनी अधिक भयभीत हो गयी कि उसका मनोबल गिर गया और वह क्रान्तिकारियों को समुचित सहयोग नहीं दे सकी।
11. नौसैनिक शक्ति का अभाव – 1857 ई० के विद्रोह को दबाने के लिए विश्व में फैले ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों से एक लाख से भी अधिक सैनिक भारत भेजे गये थे। क्रान्तिकारियों के पास कोई नौसैनिक शक्ति नहीं थी, फलत: (UPBoardSolutions.com) ये इंग्लैण्ड से आ रही युद्ध-सामग्री और सेना को रोक न सके।
![]()
प्रश्न 3.
1857 ई० के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दो प्रमुख नेताओं के जीवन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। [2014]
या
महारानी लक्ष्मीबाई कौन थीं ? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2010]
या
सन् 1857 ई० के स्वतन्त्रता संघर्ष के चार क्रान्तिकारियों का उल्लेख कीजिए। उनमें से किन्हीं दो का अंग्रेजों के प्रति असन्तोष और उनके द्वारा किये गये संघर्ष का विवरण दीजिए।
या
रानी लक्ष्मीबाई कौन थी ? उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष क्यों किया ?
या
सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के किन्हीं दो क्रान्तिकारियों के अंग्रेजों के प्रति असन्तोष और उनके संघर्ष पर प्रकाश डालिए। [2012]
या
देश के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी? संक्षेप में लिखिए। [2016]
उत्तर :
सन् 1857 ई० के स्वतन्त्रता संग्राम में अनेक क्रान्तिकारियों (नेताओं) ने उल्लेखनीय योगदान दिया, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं
1. नाना साहब – नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम धुन्धुपन्त था। अंग्रेजों ने इन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा इनकी 80 हजार पौण्ड की पेंशन बन्द कर दी। इससे नाना साहब के मन में अंग्रेजों के प्रति असन्तोष फैल गया तथा वे उनके सबसे बड़े शत्रु बन गये। हिन्दू उन्हें बाजीराव का कानूनी उत्तराधिकारी समझते थे तथा उनके प्रति अंग्रेजों का यह व्यवहार अन्यायपूर्ण समझा गया। नाना साहब ने विद्रोहियों में स्वयं को एक नायक प्रमाणित किया। अजीमुल्ला खान ने उनकी सहायता की। अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए नाना साहब ने (UPBoardSolutions.com) मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दी और स्वतन्त्रता के संघर्ष को राष्ट्रीय जागृति के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। फलत: नाना साहब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का नेतृत्व करने वालों में आगे आ गये। संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ अनेक अंग्रेज मौत के घाट उतार दिये। कुछ समय पश्चात् ही कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर वे अंग्रेजों से पराजित हो गये। क्रान्ति समाप्त होने
के बाद 1859 ई० में वे नेपाल चले गये।
2. महारानी लक्ष्मीबाई – महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी के राजा गंगाधर राव की महारानी थीं। राजा गंगाधर राव की सन् 1853 ई० में मृत्यु हो गयी। अपने पति की मृत्यु के बाद, उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन-कार्य प्रारम्भ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद-निषेध नियम का लाभ उठाकर झाँसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे महारानी असन्तुष्ट हो गयीं तथा अंग्रेजों के प्रति उनके मन में असन्तोष व्याप्त हो गया। उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी वीरता के साथ लोहा लिया तथा 1858 ई० में कालपी के निकट हुए संग्राम में वीरगति प्राप्त की।
3. मंगल पाण्डे – मंगल पाण्डे बैरकपुर की छावनी में कार्यरत एक वीर सैनिक था। इसने सबसे पहले 6 अप्रैल, 1857 ई० को चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। जब कारतूसों के प्रयोग के लिए उससे जबरदस्ती की गयी तो वह भड़क उठा और उसने शीघ्र ही दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। उस पर हत्या का आरोप लगा, परिणामस्वरूप उसे मृत्युदण्ड दिया गया। 8 अप्रैल, 1857 ई० को मंगल पाण्डे को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पाण्डे का बलिदान 1857 ई० की महाक्रान्ति का तात्कालिक कारण बना।
4. कुँवर सिंह – कुंवर सिंह बिहार प्रान्त में आन्दोलन की रणभेरी बजाने वाले महान् स्वतन्त्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। इन्होंने आजमगढ़ और बनारस में सफलताएँ प्राप्त की। अपने युद्ध-कौशल और छापामार युद्ध-नीति द्वारा इन्होंने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये। ब्रिटिश सेनानायक मारकर ने इन्हें पराजित करने का भरसक प्रयास किया, परन्तु कुंवर सिंह गंगा पार कर अपने प्रमुख गढ़ जगदीशपुर पहुँच गये और वहाँ अप्रैल, 1858 ई० में अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गयी।
5. तात्या टोपे – तात्या टोपे स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ जाने वाले महान् सेनानी थे। ये नाना साहब के सेनापति थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ई० के स्वतन्त्रता आन्दोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकटकाल (UPBoardSolutions.com) में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी रहे। रानी द्वारा ग्वालियर के किले पर अधिकार करने में इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। रानी के वीरगति प्राप्त करने पर ये क्रान्ति की मशाल लेकर दक्षिण में पहुँचे। ये अन्तिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। एक विश्वासघाती ने इन्हें सोते समय गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों ने 15 अप्रैल, 1859 ई० को इस महान् देशभक्त को तोप से उड़वा दिया।
![]()
प्रश्न 4.
सन् 1857 ई० की क्रान्ति के क्या परिणाम हुए ? [2012]
उत्तर :
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (सन् 1857 ई०) के परिणाम
सन् 1857 ई० का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम यद्यपि असफल रहा, तथापि इसके निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े –
- इस संग्राम ने इंग्लैण्ड की सरकार का ध्यान भारत में प्रशासन की ओर दिलाया, जिससे भारत को कम्पनी के शासन के स्थान पर सीधे ताज के अधीन कर दिया गया।
- महारानी विक्टोरिया ने देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय न करने की घोषणा की तथा गोद-निषेध प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
- अंग्रेजी शिक्षा के और अधिक प्रचार और प्रसार का निर्णय लिया गया।
- अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्यवादी प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण की नीति के युग का आविर्भाव किया।
- अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीयों के मन में उनके प्रति द्वेष और बढ़ा जिससे राष्ट्रीयता की भावनाएँ प्रबल हुईं, जिसके फलस्वरूप भारतीय नेता देश को उनके चंगुल से छुड़ाकर ही चैन से बैठे।
- इस क्रान्ति ने अंग्रेजों को हिन्दू-मुस्लिम एकता की शक्ति का अनुभव करा दिया; अतः अब ब्रिटिश शासकों ने ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति अपनायी। इस नीति के कारण ही भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने भारत के राष्ट्रीय जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप भारतवासी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना स्वाधीनता संघर्ष चलाने के लिए कटिबद्ध हो गये।
- इस क्रान्ति के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश संसद ने लोकतान्त्रिक (UPBoardSolutions.com) संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया। कालान्तर में भारत एक सम्प्रभुतासम्पन्न लोकतान्त्रिक देश बन गया।
- इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप जनता के प्रति अंग्रेजों की सहानुभूति कम हो गयी। उन्होंने जनता से अलग रहने की नीति अपना ली तथा प्रशासन में भी जातीय भेदभाव बढ़ गया।
- आर० सी० मजूमदार का कथन है कि “सन् 1857 ई० की क्रान्ति से भड़की आग ने भारत में ब्रिटिश शासन को उससे अधिक क्षति पहुँचायी, जितनी कि स्वयं क्रान्ति ने पहुँचायी थी।”
- अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में भारतीयों की संख्या को कम किया गया। तोपखाने में केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों की जाति, धर्म व प्रान्त के आधार पर अलग-अलग टुकड़ियाँ बनायी गयीं, जिससे वे एक न हो सकें।
इस प्रकार प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के परिणाम बड़े व्यापक तथा दूरगामी सिद्ध हुए। इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए ग्रिफिन ने कहा है कि “प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक सौभाग्यशाली घटना थी, जिसने भारतीय गगनमण्डल को अनेक मेघों से मुक्त कर दिया था।”
![]()
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
1857 ई० के संग्राम में महिला क्रान्तिकारियों के योगदानों की चर्चा संक्षेप में कीजिए।
या
भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (सन् 1857) में निम्नलिखित में से किन्हीं दो का परिचयदेते हुए उनके योगदान का वर्णन कीजिए
(क) रानी लक्ष्मीबाई, (ख) बेगम हजरत महल तथा, (ग) रानी अवन्ती बाई। (2010)
उत्तर :
1857 ई० की क्रान्ति में महिला क्रान्तिकारियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं –
1. महारानी लक्ष्मीबाई – [संकेत–विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 के उत्तर को द्वितीय शीर्षक देखें।
2. बेगम हजरत महल – अवध में बेगम हजरत महल ने क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया। ये साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थीं। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से टक्कर ली। कुछ समय के लिए ये लखनऊ क्षेत्र को स्वतन्त्र कराने में भी सफल हुईं। बाद में जनरल कैम्पबेल की सेनाओं ने 31 मार्च, 1858 ई० को लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। बेगम हजरत महल अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ीं और वहाँ से बचकर निकल गयीं।
3. बेगम जीनत महल – सन् 1857 ई० की क्रान्ति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी, इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आन्दालेन में सक्रिय भाग लेकर सिद्ध कर दिया। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थीं। इन्होंने भी सम्राट के (UPBoardSolutions.com) साथ आन्दोलन की लड़ाई को बड़े धैर्य और साहस के साथ लड़ा। राष्ट्र की स्वतन्त्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था, तभी अपनी सुख-सुविधा को छोड़कर इन्होंने स्वयं को राष्ट्र-सेवा में समर्पित कर दिया।
4. रानी अवन्ती बाई – मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवन्ती बाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रान्ति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये। बाद में अंग्रेजों की संगठित सेना के विरुद्ध लड़ते हुए रानी ने वीरतापूर्वक वीरगति प्राप्त की।
![]()
प्रश्न 2.
महारानी के घोषणा-पत्र से ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर :
महारानी के घोषणा-पत्र से ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े –
- सन् 1857 ई० की क्रान्ति के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन कम्पनी के स्थान पर ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चला गया, जिससे कम्पनी अब भारत में अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी।
- भारत की शासन-व्यवस्था अब ब्रिटिश ‘क्राउन’ द्वारा मनोनीत वायसराय को सौंप दी गयी। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया।
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के समस्त अधिकार ‘भारत सचिव’ (Secretary of State for India) को सौंप दिये गये।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 ई० के (UPBoardSolutions.com) पिट्स इण्डिया ऐक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गयी। देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया और डलहौजी की राज्य हड़प नीति निष्प्रभावी हो गयी।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब लड़ा गया ?
उत्तर :
भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ई० में लड़ा गया।
प्रश्न 2.
अपहरण की नीति किसने लागू की? इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? [2011]
उत्तर :
अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। इसकी मुख्य विशेषता देशी राज्यों पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त करना था।
प्रश्न 3.
1857 ई० की क्रान्ति कब और कहाँ से प्रारम्भ हुई ? [2011]
उत्तर :
1857 ई० की क्रान्ति का प्रारम्भ मेरठ से 10 मई, 1857 ई० को हुआ।
![]()
प्रश्न 4.
1857 ई० के स्वाधीनता-संग्राम के चार प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। [2011, 14]
उत्तर :
1857 ई० स्वाधीनता संग्राम के चार प्रमुख नेताओं के नाम निम्नलिखित हैं –
- रानी लक्ष्मीबाई
- कुंवर सिंह
- मंगल पाण्डे तथा
- नाना साहब।
प्रश्न 5.
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की दो वीरांगनाओं के नाम लिखिए।
उत्तर :
- रानी लक्ष्मीबाई तथा
- बेगम हजरत महल; प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की दो वीरांगनाएँ हैं।
प्रश्न 6.
10 मई, 1857 ई० का स्वाधीनता संग्राम किस नगर से प्रारम्भ हुआ ?
उत्तर :
10 मई, 1857 ई० का स्वाधीनता संग्राम मेरठ से प्रारम्भ हुआ।
![]()
प्रश्न 7.
रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थीं ?
उतर :
रानी लक्ष्मीबाई झाँसी राज्य की शासिका थीं।
प्रश्न 8.
1857 ई० में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था ?
उत्तर :
सन् 1857 ई० में नाना साहब (UPBoardSolutions.com) ने क्रान्ति का नेतृत्व कानपुर से किया था।
प्रश्न 9.
मंगल पाण्डे कौन थे ? उन्हें फाँसी की सजा कब दी गयी ?
उत्तर :
मंगल पाण्डे भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्हें ब्रिटिश सेना के द्वारा क्रान्ति के लिए बैरकपुर में 8 अप्रैल, 1857 ई० को फाँसी दी गयी।
प्रश्न 10.
1857 ई० की क्रान्ति के किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
1857 ई० की क्रान्ति के दो प्रभाव निम्नलिखित हैं
- देशी राज्यों को हड़पने की नीति का अन्त हो गया।
- भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
प्रश्न 11.
सन् 1857 ई० में बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले सैनिक का नाम लिखिए।
उत्तर :
बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले सैनिक का नाम मंगल पाण्डे था।
![]()
प्रश्न 12.
बेगम हजरत महल कौन थीं ?
उत्तर :
बेगम हजरत महल अवध के अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम तथा नवाब के अवयस्क बच्चे की संरक्षिका थीं। वे बड़ी वीर और साहसी महिला थीं। इन्होंने लखनऊ में क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया और 1857 ई० के (UPBoardSolutions.com) स्वतन्त्रता संग्राम में वीरता से भाग लिया।
प्रश्न 13.
बरेली में 1857 ई० के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया ?
उत्तर :
बरेली में 1857 ई० के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया।
प्रश्न 14.
कुशासन के आधार पर सर्वप्रथम किसे गद्दी से हटाया गया ?
उत्तर :
कुशासन के आधार पर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम को गद्दी से हटाया गया।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरम्भ कहाँ से हुआ ? [2009]
(क) कानपुर से
(ख) मेरठ से
(ग) दिल्ली से
(घ) लखनऊ से
2. मंगल पाण्डे किस ब्रिटिश छावनी में सैनिक थे?
(क) झाँसी
(ख) बैरकपुर
(ग) जगदीशपुर
(घ) रामपुर
3. मंगल पाण्डे को फाँसी कब दी गई ?
(क) 6 मई, 1859 ई० को
(ख) 8 अप्रैल, 1857 ई० को
(ग) 13 मई, 1859 ई० को
(घ) 17 जून, 1858 ई० को
![]()
4. 1857 ई० के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख बलिदानी कुंवर सिंह किससे सम्बन्धित थे ?
(क) जगदीशपुर से
(ख) बैरकपुर से
(ग) अवध से
(घ) बिठूर से
5. बेगम हजरत महल सम्बन्धित थींया
या
बेगम हजरत महल का सम्बन्ध किस स्थान से था ? [2013, 16, 17]
या
बेगम हजरत महल ने स्वतन्त्रता संग्राम में कहाँ का नेतृत्व किया था ? (2015)
(क) अलीगढ़ से
(ख) कानपुर से
(ग) दिल्ली से
(घ) लखनऊ से
6. रानी अवन्ती बाई किस राज्य की रानी थी? [2011, 14, 17]
या
रानी अवन्ती बाई, जिसने 1857 ई० में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, शासक थी [2013]
(क) झाँसी की
(ख) रामगढ़ की
(ग) अवध की
(घ) जगदीशपुर की
7. भारत में अन्तिम मुगल सम्राट कौन था ? [2011, 15]
(क) बहादुरशाह
(ख) औरंगजेब
(ग) शाहआलम
(घ) सिराजुद्दौला
![]()
8. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (1857) के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? [2015]
(क) लॉर्ड कैनिंग
(ख) लॉर्ड डलहौजी
(ग) लॉर्ड नार्थब्रुक
(घ) लॉर्ड मेयो
9. भारत में गोद निषेध का सिद्धान्त किसने लागू किया था?
(क) लॉर्ड डलहौजी
(ख) लॉर्ड बैंटिंक
(ग) लॉर्ड कैनिंग
(घ) लॉर्ड मिन्टो
उत्तरमाला

Hope given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 are helpful to complete your homework.
If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.