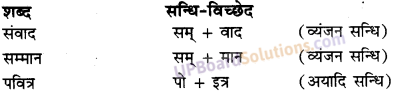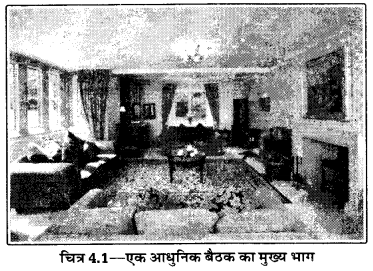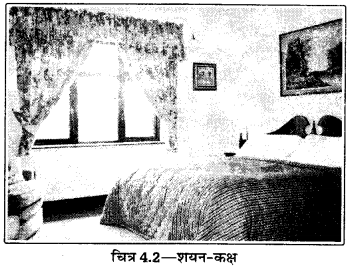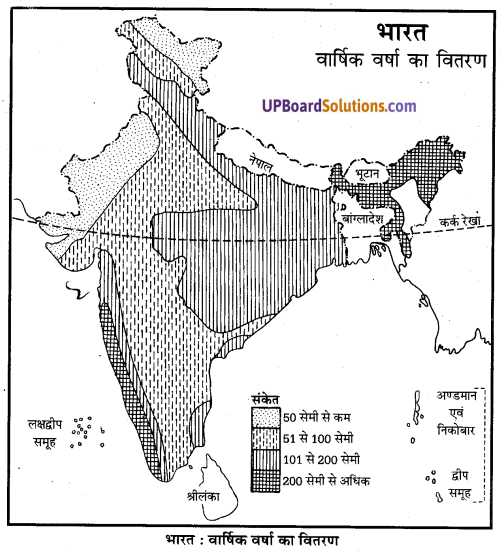UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 मानवीय संसाधन : विनिर्माणी उद्योग (अनुभाग – तीन)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 मानवीय संसाधन : विनिर्माणी उद्योग (अनुभाग – तीन).
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या महत्त्व है ? ‘आधुनिक उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए।
या
भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या महत्त्व है ?
या
देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के योगदान पर एक विशिष्ट लेख लिखिए।
उत्तर :
भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्त्व आधुनिक अर्थशास्त्री औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को पर्यायवाची मानते हैं। उनका मानना है कि उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक विकास में तेजी नहीं आ सकती। उद्योगों के समुचित विकास के बिना राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि करना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास (UPBoardSolutions.com) का अत्यधिक महत्त्व है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप भारत ने कृषि के साथ-साथ उद्योग-धन्धों के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की।
आधुनिक उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
औद्योगिक विकास किसी भी देश के विकास की गति का सूचक होता है। आज कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश भी औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। आधुनिक उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित रूपों में प्रभाव पड़ा है
1. कृषि का विकास – उद्योगों की स्थापना के पूर्व भारतीय कृषि पिछड़ी दशा में थी। उद्योगों के विकास से विशेषत: उर्वरक, कीटनाशकों, मशीनरी, कृषि उपकरण, टूक निर्माण आदि के कारण कृषि उन्नत हो गयी है। उद्योगों के ही विकास से कृषि में हरित क्रान्ति सम्भव हो सकी है।

2. नगरीकरण में वृद्धि – औद्योगीकरण तथा नगरीकरण साथ-साथ चलते हैं। उद्योगों की स्थापना से अनेक नये नगर स्थापित हो जाते हैं तथा छोटे नगरों के आकार में वृद्धि होती है। भारत के प्रायः सभी महानगर औद्योगिक विकास से ही विकसित हुए हैं।
3. रोजगार के अवसरों में वृद्धि – उद्योगों से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, पिछड़े हुए क्षेत्रों की निर्धनता दूर होती है तथा उनका आर्थिक विकास होता है।
4. राष्ट्रीय आय में वृद्धि – आधुनिक उद्योगों के कारण देश की आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
5. विदेशी व्यापार में वृद्धि – विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा विकास उद्योगों के कारण ही सम्भव हुआ है। उद्योगों की स्थापना के पूर्व भारत केवल कृषि-परक वस्तुओं तथा कच्चे माल का निर्यात करता था, किन्तु औद्योगिक विकास के कारण अब वह विनिर्मित वस्तुओं, मशीनरी आदि का भी निर्यात करने लगा है।
6. परिवहन के साधनों में वृद्धि – औद्योगिक विकास से (UPBoardSolutions.com) जनसंख्या की सघनता में वृद्धि होती है। उसके आवागमन के लिए परिवहन के साधनों में वृद्धि होती है, जो आर्थिक प्रगति का सूचक है।
7. बहुमुखी विकास – आर्थिक समृद्धि बढ़ने पर देश में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में भी विकास होता है।
कृषि पर आधारित उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका महत्त्व
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि तथा उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का विकास एक-दूसरे पर निर्भर करता है। कृषि के विकास के लिए आवश्यक वस्तुएँ; जैसे-रासायनिक खाद, औजार, ट्रैक्टर, कीटनाशक आदि उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं।
उद्योगों को कच्चा माल; जैसे—कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबड़ आदि कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी व खाण्डसारी उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग, तेल उद्योग आदि कृषि पर
आधारित उद्योग हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर आधारित उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है–
- भारत में बेकारी और अर्द्धबेकारी पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। कृषि पर आधारित उद्योग इस बेकारी को कम कर सकते हैं; क्योकि इन उद्योगों को छोटे पैमाने पर भी कम पूँजी लगाकर चलाया जा सकता है।
- कृषि पर आधारित उद्योग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल हैं। ये उद्योग देश की राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- कृषि पर आधारित उद्योगों से कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी आती है और बहुत-से लोगों को रोजगार मिलता है।
- इन उद्योगों से बड़े उद्योगों को सहायता (UPBoardSolutions.com) मिलती है।
- इन उद्योगों से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा निर्यातों में वृद्धि के आयातों में कमी होती है।
- कृषि पर आधारित उद्योगों से देश में औद्योगीकरण के विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रश्न 2.
भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं ? प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योगों का विवरण दीजिए।
उत्तर :
इंजीनियरिंग उद्योग
इंजीनियरिंग उद्योगों में अनेक विनिर्माण उद्योग सम्मिलित होते हैं; जैसे-औजार व मशीनें बनाने वाले उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, परिवहन उपकरण उद्योग; जैसे-रेल इंजन उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग, मोटर उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग आदि। भारत में इन उद्योगों का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। यहाँ इनमें से अधिकांश उद्योगों को आधारभूत उद्योग की सूची में सम्मिलित किया हुआ है तथा इनमें से अनेक इंजीनियरिंग उद्योग सरकारी क्षेत्र में चलाये जा रहे हैं।
भारी मशीनरी उद्योग
देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास 1958 ई० में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (राँची) की स्थापना के पश्चात् हुआ। इसकी तीन इकाइयाँ हैं–
- भारी मशीनरी निर्माण संयन्त्र,
- फाउण्ड्री फोर्ज संयन्त्र तथा
- भारी मशीन उपकरण (HMT) संयन्त्र।
विशिष्ट प्रकार के इस्पात के ढाँचों का डिजाइन बनाने का कारखाना 1965 ई० में ऑस्ट्रिया के सहयोग से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी (इलाहाबाद) में स्थापित हुआ। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि० 1947 ई० में तुंगभद्रा (कर्नाटक) में स्थापित हुआ था। निजी क्षेत्र में मुम्बई में लार्सन एण्ड टुब्रो लि०, गेस्ट-कीन एवं विलियन एण्ड ग्रीव्ज़ कॉटन स्थापित हैं। सन् 1966 ई० में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से भारत हेवी प्लेट एण्ड (UPBoardSolutions.com) वेसल्स लि०, विशाखापत्तनम् स्थापित हुआ। यहाँ उर्वरक, पेट्रो रसायन तथा अनेक सम्बद्ध उद्योगों की मशीनरी तैयार होती है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग के अन्तर्गत क्रेन, इस्पात के ढाँचे, ट्रांसमिशन टॉवर, ढलाई में काम आने वाले उपकरण आदि बनाये जाते हैं। दुर्गापुर में स्थापित माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लि० (MAMC) खनन में काम आने वाली मशीनरी तैयार करता है। औद्योगिक मशीनरी के उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। टेक्सटाइल मशीनरी का निर्माण करने वाला निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना टेक्समैको (TEXMACO) मुम्बई में 1939 ई० में स्थापित किया गया था।

मशीनों के उपकरण उद्योग
भारत में गत वर्षों में मशीनों के औजार बनाने में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। इस कार्य में है 700 करोड़ वार्षिक क्षमता की 200 इकाइयाँ संलग्न हैं। बड़े कारखाने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (HMT) बंगलुरु के अतिरिक्त पिंजौर (हरियाणा), कलामासेरी (केरल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा श्रीनगर (कश्मीर) में हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रकार की मशीनें तथा सूक्ष्म वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। सेण्ट्रल मशीन टूल्स इन्स्टीट्यूट, बंगलुरु (UPBoardSolutions.com) की स्थापना 1965 ई० में की गयी थी। यहाँ मशीनरी औजारों के क्षेत्र में अनुसन्धान किये जाते हैं। मशीन टूल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, अजमेर की स्थापना 1967 ई० में की गयी थी। यहाँ घिसाई के काम आने वाले मशीनी औजार तैयार किये जाते हैं। हेवी मशीन टूल प्लाण्ट (राँची) में धुरी तथा पहिये तैयार किये जाते हैं। प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन लि० (सिकन्दराबाद) भी मशीनों के उपकरण तैयार करता है।
परिवहन उपकरण उद्योग
(i) रेल इंजन उद्योग – स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत रेल इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर था। अतः 1947 ई० के बाद भारत ने देश में ही रेल इंजन बनाने की दिशा में कार्य आरम्भ किये, जिनका विवरण निम्नलिखित है–
चितरंजन–सन् 1948 ई० में भारत सरकार ने रेल के इंजनों का एक बहुत बड़ा कारखाना पश्चिमी बंगाल में चितरंजन नामक स्थान पर लगाया। यहाँ भाप के इंजनों का निर्माण किया जाता था, किन्तु 1981 ई० में इस कारखाने ने भाप के इंजन बनाने (UPBoardSolutions.com) बन्द कर दिये। अब यह कारखाना बिजली तथा डीजल के इंजनों का निर्माण कर रहा है।
वाराणसी-उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित इस कारखाने में केवल डीजल इंजन बनाये जाते हैं। यह कारखाना प्रति वर्ष 150 डीजल इंजन बनाती है।

(ii) रेल पटरियाँ, वैगन एवं कोच – रेल की पटरियाँ बनाने में हिन्दुस्तान स्टील लि० (HSL), टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO), इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (ISCO) संलग्न हैं।
वैगन तथा कोच बनाने का कार्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में किया जाता है। इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर (ICF), चेन्नई के निकट 1955 ई० में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की गयी। यहाँ विविध प्रकार के कोच (वातानुकूलित, विद्युत तथा डीजल रेल, कार आदि) तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेलकोच फैक्ट्री (कपूरथला) में मार्च, 1988 ई० में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। डीजल कम्पोनेण्ट वर्क्स (DCw), पटियाला में डीजल इंजनों के पुर्जे आदि तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रकार, अब भारत रेल इंजनों के बारे में पूर्णतया आत्मनिर्भर है।
(iii) वायुयान-निर्माण उद्योग – द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत में वायुयान बनाने का कोई भी कारखाना नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसे कारखानों की आवश्यकता अनुभव की गयी। सन् 1940 ई० में मैसूर सरकार व बालचन्द हीराचन्द नामक एक फर्म की सम्मिलित साझेदारी में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी’ के नाम से हवाई जहाज बनाने का एक कारखाना बंगलुरु (कर्नाटक) में खोला गया। सन् 1942 ई० में सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम ‘हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (HAL) रखा गया। इसकी इकाइयाँ बंगलुरु, कानपुर, नासिक, कोरापुट, हैदराबाद तथा कोरवा (लखनऊ) में स्थापित हैं।
पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस से तकनीकी जानकारी प्राप्त करके (UPBoardSolutions.com) अब देश में ही मिग, जगुआर, चीता, चेतक जैसे वायुयान, लड़ाकू विमान तथा हेलिकॉप्टर तैयार किये जा रहे हैं।
(iv) जलयान-निर्माण उद्योग – भारत में तीन हजार किलोमीटर लम्बा विशाल समुद्रतट है; अत: देश की सुरक्षा तथा विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत को बड़ी मात्रा में जलयानों की आवश्यकता होती है; किन्तु विदेशी शासन काल में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस समय भारत में पाँच बड़े पोत निर्माण केन्द्र–मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, विशाखापत्तनम् तथा गोआ हैं।
विशाखापत्तनम् – सन् 1941 ई० में सिंधिया कम्पनी ने जलयान निर्माण का पहला कारखाना आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम् बन्दरगाह पर खोला। सन् 1947 ई० में भारत सरकार ने इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नाम हिन्दुस्तान शिपयार्ड रखा। सन् 1948 ई० में इसमें सबसे पहला जलयान बना और अब तक इसमें 86 जलयान बन चुके हैं।
कोच्चि – पश्चिमी तट पर केरल राज्य में कोच्चि बन्दरगाह पर भी जापान के सहयोग से एक जलयान का कारखाना स्थापित किया गया है। सन् 1979 ई० से इसमें जहाज बनने शुरू हो गये हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में ‘गार्डन रीच जहाजी कारखाने में समुद्री व्यापारिक जहाजों तथा मझगाँव (मुम्बई) स्थित जहाजी कारखाने में नौ-सेना के लिए फिगेट जहाजों का निर्माण किया जाता

प्रश्न 3.
भारत में चीनी उद्योग का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में किंन्हीं तीन राज्यों के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। [2014]
या
भारत में चीनी उद्योगं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए
(क) उत्पादक क्षेत्र/राज्य तथा (ख) उत्पादन एवं व्यापार।
उत्तर :
भारत में चीनी उद्योग
चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। भारत में गन्ने से गुड़, शक्कर तथा खाँड बनाने का व्यवसाय (खाँडसारी उद्योग) बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है, किन्तु आधुनिक विधि से. चीनी बनाने का उद्योग बीसवीं शताब्दी से ही उन्नत हो पाया है। इससे पूर्व वर्ष 1841-42 में उत्तरी बिहार में डच लोगों तथा सन् 1899 ई० में अंग्रेजों द्वारा चीनी की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के असफल प्रयास किये गये थे। इस उद्योग का वास्तविक आरम्भ सन् 1930 ई० से हुआ।
सन् 1931 ई० तक चीनी उद्योग के विकास की गति बहुत धीमी रही और प्रचुर मात्रा में चीनी का आयात विदेशों से किया जाता रहा। सन् 1931 ई० में केवल 31 चीनी की फैक्ट्रियाँ कार्यरत थीं, जिनको उत्पादन 6.58 लाख टन था। सन् 1932 ई० में इस उद्योग की सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया और तभी से चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। संरक्षण के 4 वर्ष बाद मिलों की संख्या बढ़कर 35 हो गयी और चीनी का उत्पादन बढ़कर 9.19 लाख टन हो गया। वर्ष 1938-39 में इनकी संख्या बढ़कर 132 हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीनी की माँग बढ़ जाने के कारण चीनी के मूल्य तेजी से बढ़ने आरम्भ हो गये। अतएव सरकार ने सन् 1942 ई० में इसके मूल्य पर नियन्त्रण लगा दिया तथा इसकी राशनिंग आरम्भ कर दी। सन् 1950 ई० में चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। वर्ष 1991-92 में देश में 370 चीनी के कारखाने थे। वर्ष 1998 में देश में चीनी मिलों की संख्या 465 तक पहुँच गयी, जिनमें से लगभग आधी सहकारी क्षेत्र में हैं, जो कुल उत्पादन का 60% उत्पादन करती हैं। इस उद्योग में लगभग १ 1,500 करोड़ की पूँजी लगी हुई है। और लगभग 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 2006-07 में देश में चीनी का उत्पादन 281.99 लाख टेन (अस्थायी) से अधिक हो चुका था।

उत्पादक राज्य
1. महाराष्ट्र – महाराष्ट्र राज्य ने चीनी के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक प्रगति की है। चीनी के उत्पादन में इसका देश में प्रथम स्थान है। यहाँ 129 चीनी मिलें हैं जिनमें देश की लगभग 35% से भी अधिक चीनी उत्पादित की जाती है। गोदावरी, प्रवरा, मूला-मूठा, नीरा एवं कृष्णा नदियों की घाटियों में चीनी मिलें केन्द्रित हैं। मनमाड़, नासिक, पुणे, अहमदनगर, शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, सतारा एवं साँगली प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं।
2. उत्तर प्रदेश – इस राज्य का चीनी के उत्पादन में द्वितीय तथा गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। इस प्रदेश में 128 चीनी मिले हैं। प्रदेश में उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही चीनी मिलों का केन्द्रीकरण हुआ है। यह राज्य देश की 24% चीनी का उत्पादन करता है तथा यहाँ देश का सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है।
3. कर्नाटक – चीनी के उत्पादन में कर्नाटक राज्य को देश में (UPBoardSolutions.com) तीसरा स्थान है। यहाँ पर चीनी उद्योग के 37 केन्द्र हैं, जिनमें देश की 9% चीनी का उत्पादन किया जाता है। बेलगाम, मांड्या, बीजापुर, बेलारी, शिमोगा एवं चित्रदुर्ग महत्त्वपूर्ण चीनी उत्पादक जिले हैं।
4. तमिलनाडु – इस राज्य में 22 चीनी मिलें हैं। यहाँ देश की लगभग 8% चीनी उत्पादित की जाती है। मदुराई, उत्तरी एवं दक्षिणी अर्कोट, कोयम्बटूर एवं तिरुचिरापल्ली प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं।
5. बिहार – बिहार में देश की 5% चीनी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ चीनी की 40 मिले हैं, जो विशेष रूप से सारन, चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गोपालगंज आदि उत्तरी जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त चीनी उत्पादक अन्य राज्यों में गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल मुख्य हैं।
व्यापार
भारत चीनी का निर्यातक देश है और विश्व के चीनी निर्यात व्यापार में भारत 0.6% का हिस्सा रखता है। देश की आवश्यकता को पूरी करने के उपरान्त केवल 2 लाख टन चीनी निर्यात के लिए शेष बचती है, जिससे निर्यात की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 20 अगस्त, 1998 ई० को इसे लाइसेन्स व्यवस्था से मुक्त कर दिया है।

प्रश्न 4.
भारत में कागज उद्योग के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए।
या
भारत में कागज उद्योग का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण दीजिए।
या
भारत में कागज उद्योग के कच्चे माल की उपलब्धता एवं प्रमुख केन्द्रों का वर्णन कीजिए। [2013]
उत्तर :
भारत में कागज उद्योग
भारत को वर्तमान कागज उद्योग 19वीं शताब्दी की देन माना जाता है। आधुनिक ढंग की प्रथम कागज मिल 1816 ई० में ट्रंकुवार (चेन्नई के समीप) नामक स्थान पर खोली गयी, परन्तु इसे सफलता न मिल सकी। हुगली : नदी के किनारे सिरामपुर (UPBoardSolutions.com) (प० बंगाल) में स्थापित मिल को भी असफलता ही मिली। इसके पश्चात् 1867 ई० में बाली (कोलकाता) नामक स्थान पर रॉयल पेपर मिल की स्थापना हुई। इस उद्योग का वास्तविक विकास तब हुआ जब 1879 ई० में लखनऊ में अपर इण्डिया पेपर मिल्स तथा 1881 ई० में पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना की गयी। इसके बाद कारखानों की संख्या में वृद्धि होती गयी।
वर्तमान में भारत में गत्ता एवं कागज की 759 इकाइयाँ हैं, जिनमें से केवल 651 चालू हालत में हैं और 2,748 लघु इकाइयाँ उत्पादन में संलग्न हैं। कुल स्थापित क्षमता लगभग 128 लाख टन है, किन्तु रुग्णता (बीमार) के कारणं बहुत-सी कागज मिलें बन्द पड़ी हैं। इसलिए उत्पादन क्षमता घटकर 60 प्रतिशत ही रह गयी है। पेपर और पेपर बोर्ड क्षेत्र में भारत सक्षम है। पारंपरिक तौर पर स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कागजों का आयात करना पड़ता है। वर्ष 2010-11 में कागज बोर्ड का उत्पादन 7.37 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष 7.06 मिलियन टन था।
कागज और कागज बोर्ड का 2010-11 के दौरान कुल आयात (न्यूज प्रिंट छोड़कर) 0.72 मिलियन टन रही। 2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) में यह 0.72 मिलियन टन रहा।
न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में 113 मिलें सूचीबद्ध हैं। इन्हें उत्पाद शुल्क से छूट मिली हुई है। इस समय 68 मिलें न्यूजप्रिंट का उत्पादन करती हैं, जिनकी प्रचालन स्थापित क्षमता 1.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। एनसीओ में सूचीबद्ध किये जाने के बाद 20 मिलों ने काम करना बंद कर दिया है और 25 ने न्यूजप्रिंट का उत्पादन रोक दिया है।
उत्पादन एवं वितरण
कागज के उत्पादन की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के मुख्य 15 कागज-निर्माताओं में की जाती है। देश के 70% से भी अधिक कागज का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश राज्यों में होता है। प्रमुख कागज उत्पादक राज्यों का विवरण इस प्रकार है-

1. पश्चिम बंगाल – यहाँ देश का लगभग 20% कागज का उत्पादन होता है। राज्य में कागज की 19 मिले हैं। टीटागढ़, नैहाटी, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता, काकीनाड़ा, चन्द्रहाटी (हुगली), आलम बाजार (कोलकाता), बड़ानगर, बाँसबेरिया तथा शिवराफूली कागज उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। टीटागढ़ में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है, जिसमें बाँस का कागज निर्मित किया जाता है।
2. महाराष्ट्र – यहाँ 14 कागज ऐवं 3 कागज-गत्ते के सम्मिलित कारखाने हैं, जो देश के लगभग 13% कागज का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर कोमल लकड़ी की लुगदी विदेशों से आयात की जाती है। इसके अतिरिक्त बाँस, खोई एवं फटे-पुराने चिथड़ों का उपयोग कागज (UPBoardSolutions.com) बनाने में किया जाता है। गन्ने की खोई एवं धान की भूसी से गत्ता बनाया जाता है। पुणे, खोपोली, मुम्बई, बलारपुर, चन्द्रपुर, ओगेलवाडी, चिचवाडा, रोहा, कराड़, कोलाबा, कल्याण, वाड़ावाली, काम्पटी, नन्दुरबाद, पिम्परी, भिवण्डी एवं वारसनगाँव कागज उद्योग के प्रधान केन्द्र हैं। बलारपुर एवं साँगली में अखबारी कागज की मिलें भी स्थापित की गयी हैं।
3. आन्ध्र प्रदेश – यहाँ देश का 12% कागज तैयार किया जाता है। कागज उद्योग के लिए बाँस इस राज्य का प्रमुख कच्चा माल है। सिरपुर, तिरुपति तथा राजमुन्दरी प्रमुख कागज उत्पादक केन्द्र हैं।
4. मध्य प्रदेश – इस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ बाँस एवं सवाई घास पर्याप्त मात्रा में उगती है। यहाँ देश का 10% कागज तैयार किया जाता है। इस राज्य में इन्दौर, भोपाल, सिहोर, शहडोल, रतलाम, मण्डीदीप, अमलाई एवं विदिशा प्रमुख कागज उत्पादक केन्द्र हैं। नेपानगर में अखबारी कागज
(1955 ई०) तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना स्थापित है।
5. कर्नाटक – यहाँ देश का 10% कागज बनाया जाता है। इस राज्य में भद्रावती, बेलागुला तथा डाँडली केन्द्रों पर कागज की मिलें हैं।
6. उत्तर प्रदेश – इस राज्य का कागज उद्योग शिवालिक एवं तराई क्षेत्रों में सवाई, भाबर एवं मूंज घास तथा बाँस की प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देश का लगभग 4% कागज उत्पन्न किया जाता है। लखनऊ, गोरखपुर एवं सहारनपुर कागज उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर, उझानी, पिपराइच, मोदीनगर, नैनी, लखनऊ तथा सहारनपुर प्रमुख गत्ता उत्पादक केन्द्र हैं। भारत के अन्य (UPBoardSolutions.com) कागज उत्पादक राज्यों में बिहार, गुजरात, ओडिशा, केरल, हरियाणा एवं तमिलनाडु प्रमुख हैं।
प्रश्न 5.
भारत के सीमेण्ट उद्योग का विस्तपूर्वक वर्णन कीजिए। [2010]
या
भारत में सीमेण्ट उद्योग कहाँ स्थापित हैं ? एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए।
या
भारत में सीमेण्ट उद्योग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए- [2011]
(क) केन्द्र, (ख) उत्पादन तथा (ग) व्यापार
उत्तर :
भारत में सीमेण्ट उद्योग
किसी भी विकासोन्मुख राष्ट्र के लिए सीमेण्ट का अत्यधिक महत्त्व है। प्रत्येक प्रकार के भवन-निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। भारत में संगठित रूप से सीमेण्ट तैयार करने का प्रथम प्रयास चेन्नई में 1904 ई० में किया गया था, परन्तु इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। इस उद्योग का वास्तविक विकास 1914 ई० में हुआ, जब कि मध्य प्रदेश में कटनी, राजस्थान में लखेरी-बूंदी तथा गुजरात में पोरबन्दर में तीन कारखाने स्थापित किये गये। सीमेण्ट वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सीमेण्ट उद्योग का विकास अति आवश्यक है। यह अनेक उद्योगों के विकास की कुंजी है। भारत संसार का चौथा बड़ा सीमेण्ट उत्पादक देश है। अप्रैल, 2003 ई० को देश में 124 बड़े सीमेण्ट संयन्त्र थे, जिनकी संस्थापित क्षमता लगभग 14 करोड़ टन (UPBoardSolutions.com) थी। सीमेण्ट अनुसन्धान संस्थान ने देश में लघु सीमेण्ट संयन्त्र लगाने के सुझाव दिये हैं। इससे प्रेरित होकर विभिन्न राज्यों में 300 लघु संयन्त्र स्थापित किये हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 111 लाख टन वार्षिक है। 31 मार्च, 2012 तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार देश में 173 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं जिनकी स्थापित क्षमता 294.04 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जबकि 350 छोटे सीमेण्ट संयंत्र हैं। जिनकी स्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन/वर्ष है और कुल स्थापित क्षमता 305.14 मिलियन टन प्रतिवर्ष कुछ बड़े सीमेण्ट संयंत्रों का स्वामित्व केन्द्र और राज्य सरकारों के पास है।

उत्पादन एवं वितरण
सीमेण्ट उद्योग देशभर में विकेन्द्रित है। अधिकांश कारखाने देश के पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में विकसित हुए हैं, जब कि सीमेण्ट की अधिकांश माँग उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में अधिक है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश राज्य देश का 74% सीमेण्ट उत्पन्न करते हैं, जब कि कुल उत्पादित क्षमता का 86% भाग इन्हीं राज्यों में केन्द्रित है। अग्रलिखित राज्यों का सीमेण्ट उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान है
1. मध्य प्रदेश – सीमेण्ट उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ सीमेण्ट के आठ विशाल कारखाने तथा कई लघु संयन्त्र कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश राज्य देश का 15% सीमेण्ट उत्पन्न कर प्रथम स्थान पर है। इस राज्य में सीमेण्ट उद्योग के लिए आधारभूत सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध है तथा कोयला झारखण्ड से मँगवाया जाता है। इस राज्य के कटनी, कैमूर, सतना, जबलपुर, बनमोर, नीमच एवं दमोह में सीमेण्ट के प्रमुख कारखाने हैं।
2. तमिलनाडु – यहाँ सीमेण्ट के 8 बड़े कारखाने हैं, जो देश का 12% सीमेण्ट उत्पन्न करते हैं। सीमेण्ट उत्पादन में इस राज्य का दूसरा स्थान है। चूना-पत्थर की पूर्ति स्थानीय क्षेत्रों के साथ-साथ कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों से भी की जाती है। तुलुकापट्टी, तिलाईयुथू, तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, राजमलायम, संकरी दुर्ग एवं मधुकराई प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं।
3. आन्ध्र प्रदेश – आन्ध्र प्रदेश में सीमेण्ट के 11 कारखाने एवं 12 लघु संयन्त्र हैं, जो गुण्टूर, कर्नूल, नालगोण्डा, मछलीपत्तनम्, हैदराबाद एवं विजयवाड़ा में केन्द्रित हैं। इस राज्य में चूना-पत्थर के विशाल भण्डार पाये जाते हैं, इसी कारण इस राज्य (UPBoardSolutions.com) की सीमेण्ट उत्पादन क्षमता 45 लाख टन तक पहुँच गयी है। सीमेण्ट उत्पादन में इस राज्य का तीसरा स्थान है।
4. राजस्थान – सीमेण्ट के उत्पादन में राजस्थान राज्य का चौथा स्थान है। यहाँ अरावली पहाड़ियों में । चूने-पत्थर व जिप्सम के पर्याप्त भण्डार हैं। ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेण्ट उत्पादक राज्य हो जाएगा। यहाँ सीमेण्ट उत्पादन के 10 कारखाने हैं, जिनमें देश का 10% सीमेण्ट निर्मित किया जाता है। लखेरी (बूंदी), सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू,. निम्बाहेड़ा एवं उदयपुर सीमेण्ट उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं।
5. झारखण्ड – झारखण्ड सीमेण्ट उत्पादक राज्यों में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ डालमियानगर, सिन्द्री, बनजोरी, चौबासा, खलारी, जापला एवं कल्याणपुर प्रमुख केन्द्र हैं।
6. कर्नाटक – इस राज्य में बीजापुर, भद्रावती, गुलर्गा, उत्तरी कनारा, तुमुकुर एवं बंगलुरु प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं। यहाँ सीमेण्ट उत्पादन के 6 बड़े संयन्त्र स्थापित किये गये हैं।
7. गुजरात – गुजरात राज्य में सीमेण्ट के 8 कारखाने हैं। सीमेण्ट उद्योग का प्रारम्भ इसी राज्य से किया गया था। सिक्का (जामनगर), अहमदाबाद, राणाबाव, बड़ोदरा, पोरबन्दर, सेवालिया, ओखामण्डल एवं द्वारका प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं।

8. छत्तीसगढ़ – यहाँ सीमेण्ट के कुछ कारखाने हैं जिनमें दुर्ग व गन्धार के कारखाने मुख्य हैं।
9. अन्य राज्य – हरियाणा में सूरजपुर एवं डालमिया-दादरी; केरल (UPBoardSolutions.com) में कोट्टायम; उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं चोपन; ओडिशा में राजगंगपुर एवं हीराकुड; जम्मू-कश्मीर में वुयान तथा असम में गौहाटी अन्य प्रमुख सीमेण्ट उत्पादक केन्द्र हैं।
व्यापार
भारत के सीमेण्ट उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कुल उत्पादन-क्षमता का 84% सीमेण्ट को उत्पादन किया जाता है। सन् 1965 ई० में इस उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु सीमेण्ट निगम की स्थापना की गयी थी। इस निगम का प्रमुख कार्य कच्चे माल के नये क्षेत्रों का पता लगाना तथा इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को हल करना था। वर्तमान समय में हम सीमेण्ट उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गये हैं। वर्ष 2004-05 में 78.3 लाख टन सीमेण्ट का निर्यात भी किया गया था। बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि हमारे सीमेण्ट के प्रमुख ग्राहक हैं।
वर्ष 2010-11 के दौरान सीमेंट उत्पादन (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक) 224.49 मिलियन टन हुआ और 2010-11 की इसी अवधि तुलना में 6.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने अप्रैल, 2011-12 के दौरान 3.86 मिलियन टन सीमेंट और खंगरों का निर्यात किया है। इस क्षेत्र में प्रचुर माँग और ज्यादा लाभ उद्योग के विकास के अनुकूल है। यह उद्योग 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 100 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि की योजना थी लेकिन इस अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि 126.25 मिलियन टन की हुई।
प्रश्न 6.
भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राम उद्योगों की समस्याएँ बताइए तथा उनके हल के लिए उपाय सुझाष्ट।
उत्तर :
भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राम उद्योगों की समस्याएँ ग्रामीण उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ अग्र हैं
- इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं उपलब्ध हो पाता। जो माल इन्हें प्राप्त होता है वह अच्छी किस्म का नहीं होता।
- बैंकों से ऋण मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल हैं कि इन्हें मजबूर होकर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है।
- उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए नियमित बाजार न होने से इन उद्योगों का विकास अवरुद्ध हुआ है।
- ग्रामीण उद्योगों को बड़े उद्योगों में बनी वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े उद्योगों की वस्तुएँ सस्ती एवं आकर्षक होती हैं, जिससे इन्हें अपनी वस्तुएँ बेचने में कठिनाई होती है।
- इन उद्योगों को चलाने के लिए कुशल प्रबन्धक नहीं मिल पाते।
- इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर आज भी पुराने औजारों एवं पुरानी पद्धतियों के अनुसार कार्य करते हैं जिनसे कम उत्पादन प्राप्त होता है।
- इन उद्योगों के कारीगर इतने गरीब होते हैं कि वे नवीन यन्त्रों और औजारों को नहीं खरीद पाते, जिससे सस्ती एवं अच्छी वस्तु नहीं बन पाती।
- इनमें काम करने वाले शिल्पकारों का कोई सामूहिक संगठन नहीं है, जिससे इनमें सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का अभाव पाया जाता है।

ग्राम उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव
ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं
- कच्चे माल की व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँ जिसमें सहकारी सहयोग की आवश्यकता होती है।
- शिल्पकारों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाए, जिससे उनकी सामूहिक क्रयशक्ति में वृद्धि की जा सके।
- तैयार माल के क्रय-विक्रय में इन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- उत्पादन विधियों में सुधार करने तथा आधुनिक ढंगों को अपनाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।
- कारीगरों को आधुनिक यन्त्रों एवं औजारों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की जाए।
- ग्रामीण उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचना आवश्यक है।
- ग्रामीण उद्योग के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।
- इन उद्योगों की सुरक्षा के लिए अनेक बोर्डो और निगमों (UPBoardSolutions.com) की स्थापना की गयी है; जैसे-अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि।
- 2 अप्रैल, 1990 को लघु उद्योगों को ऋण देने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गयी।
- 2000-01 में नयी ऋण नीति में मिश्रित ऋण सीमा को 25 लाख के ऊपर तक बढ़ाया गया। ऋण गारण्टी योजना को लागू किया गया।
प्रश्न 7.
उत्तर भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख तीन कारणों की समीक्षा कीजिए। मध्य भारत में इस उद्योग के लगाने में प्रमुख दो बाधाओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
उत्तर भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण
- कच्चे माल के रूप में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन।
- अनुकूल जलवायु
- शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता।
- सस्ते एवं कुशल श्रम की बहुलता।
- परिवहन के सस्ते साधनों की उपलब्धता।
- व्यापक बाजार।

मध्य भारत में चीनी उद्योग स्थापित करने में आने वाली बाधाएँ मध्य भारत में चीनी उद्योग को स्थापित करने में आने वाली दो प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं
1. श्रमिकों की अनुपलब्धता – गन्ने की एक फसल 10-12 महीनों में तैयार होती है। गन्ने के लिए खेत तैयार करने, बोने, निराई-गुड़ाई करने तथा उन्हें काटकर मिलों तक पहुँचाने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता होती है। इसी कारण से गन्ना सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। मध्य भारत के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में भौगोलिक स्थितियों के कारण जनसंख्या अत्यधिक विरल है, अतः श्रमिकों की अनुपलब्धता है, जो कि इस उद्योग के स्थापित होने में प्रमुख रूप से बाधक है।
2. उपयुक्त मृदा की अनुपलब्धता – गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट तथा नमीयुक्त गहरी– चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। यह मिट्टी से अधिक पोषक तत्त्व भी ग्रहण करता है। इसलिए इसे अतिरिक्त खाद की भी आवश्यकता होती है। मध्य भारत (UPBoardSolutions.com) के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में न तो गन्ने की उपज के लिए अनुकूल उपजाऊ मृदा उपलब्ध है और न ही खादों की आपूर्ति सुगम है। यही कारण इस उद्योग के स्थापित होने में बाधक हैं।। उपर्युक्त दोनों कारणों से भी अधिक गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, परिवहन के साधन, समुचित वर्षा, सिंचाई के साधनों का अभाव आदि मध्य भारत में इस उद्योग को स्थापित करने में प्रमुख रूप से बाधक हैं।
प्रश्न 8.
भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण की विवेचना कीजिए। [2018]
या
भारत में तीन प्रदेशों के सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्रों का वर्णन कीजिए। [2014, 17]
या
भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास का कच्चे माल की उपलब्धता एवं उसके प्रमुख केन्द्रों के साथ वर्णन कीजिए।
उत्तर :
भारत में सूती वस्त्र उद्योग
भारत में सूती वस्त्रों के उपयोग की परम्परा बहुत प्राचीन है। सिन्धु सभ्यता में बने वस्त्रों की माँग यूरोपीय और मध्य-पूर्व के देशों में बहुत अधिक थी। उस काल में सूती वस्त्र उद्योग ग्रामीण या कुटीर उद्योग के रूप में संचालित किया जाता था। वस्त्र के (UPBoardSolutions.com) लिए धागा बनाने की मशीन मात्र चरखा थी। उन्नीसवीं शताब्दी के
आरम्भिक वर्षों में कोलकाता के निकट सूती मिल की स्थापना की गई। परन्तु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन् 1954 ई० से प्रारम्भ हुआ, जब पूर्ण रूप से भारतीय पूँजी द्वारा मुम्बई में सूती मिल की स्थापना की गई थी।
महत्त्व – सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। यह न केवल वस्त्र जैसी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करता है वरन् बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध कराता है। यह निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी कमाकर देता है।
स्थानीयकरण के कारण – भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारण हैं
- पर्याप्त कच्चे माल (कपास) का स्थानीय उत्पादन।
- अनुकूल नम जलवायु तथा स्वच्छ जल।
- रासायनिक पदार्थों का सरलता से मिलना।
- सस्ते एवं कुशल श्रमिकों का मिलना।
- परिवहन के सस्ते साधनों का मिलना।
- वस्त्र बनाने वाली मशीनरी की उपलब्धता।
- वस्त्र उद्योग को सरकारी संरक्षण तथा सहायता प्राप्त होना।
- उपभोक्ता बाजार निकट स्थित होना।
- शक्ति के पर्याप्त संसाधन मिलना।
- विदेशी सूती वस्त्रों पर भारी आयात कर का होना।
- सूती वस्त्र निर्यात की उदार सरकारी नीति का पालन करना।

उत्पादन-सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग है। यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तथा विकसित उद्योग है। यह देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% का अंशदान करता है। देश के कुल निर्यात व्यापार में लगभग 23% की हिस्सेदारी रखने वाला निर्यातपरक यह उद्योग लगभग 35 लाख लोगों की जीविका चला रहा है। भारत का विश्व के सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। (UPBoardSolutions.com) परन्तु तकुओं की दृष्टि से प्रथम स्थान है। भारत में सूती वस्त्र बनाने का कार्य पहले कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता था, परन्तु अब यह एक महत्त्वपूर्ण संगठित उद्योग के रूप में विकसित हो गया है। भारत के अनेक राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। यह क्षेत्र हैं-मुम्बई, हैदराबाद, सूरत, शोलापुर, कोयम्बटूर, नागपुर, मदुरै, कानपुर, बंगलुरु, पुणे और चेन्नई।
सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन के क्षेत्र एवं महत्त्वपूर्ण केन्द्र
यद्यपि भारत के अनेक राज्यों में सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, परन्तु इसका सर्वाधिक विकास गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में हुआ है। मुम्बई तथा अहमदाबाद नगर सूती वस्त्र उद्योग के प्रधान केन्द्र हैं। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन राज्यों का विवरण निम्न प्रकार है
1. गुजरात-सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। यह देश का लगभग 33% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अहमदाबाद महानगर सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केन्द्र है। यही कारण है कि अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बड़ोदरा, सूरत, भरूच, बिलिमोरिया, मोरवी, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, कलोल, भावनगर, नाडियाड, पोरबन्दर तथा जामनगर अन्य प्रमुख सूती वस्त्र बनाने वाले केन्द्र हैं।
2. महाराष्ट्र – इस राज्य का भारत के सूती वस्त्र उद्योग में दूसरा स्थान है। मुम्बई महानगर में खटाऊ, फिनले तथा सेंचुरी जैसी प्रसिद्ध सूती वस्त्र मिले हैं। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के अन्य केन्द्रों में शोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, सतारा, वर्धा, (UPBoardSolutions.com) अमरावती, सांगली, थाणे, जलगाँव, अकोला, सिद्धपुर, चालीसगाँव, धूलिया, औरंगाबाद आदि प्रमुख हैं।
3. तमिलनाडु – इस राज्य में कोयम्बटूर सूती वस्त्र का प्रमुख केन्द्र है। सलेम, चेन्नई, रामनाथपुरम, तूतीकोरिन, तंजावूर, मदुरै, पेराम्बूर आदि अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं।
4. उत्तर प्रदेश – यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, कानपुर महानगर इस उद्योग का मुख्य केन्द्र है, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्रों में वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, मोदीनगर, पिलखुवा, सण्डीला, इटावा आदि मुख्य हैं।
5. पश्चिम बंगाल – सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का भारत में तीसरा स्थान है। यह राज्य भारत का 15% सूती वस्त्र उत्पादित करता है। कच्चे माल की कमी आयातित कपास से पूरी की जाती है। चौबीस-परगना, हावड़ा एवं हुगली प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन जिले हैं। कोलकाता, श्रीरामपुर, हुगली, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, रिशरा, फूलेश्वर, धुबरी आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र हैं।
अन्य राज्य – भारत के अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, बिहार एवं दिल्ली प्रमुख हैं।
व्यापार – भारत सूती वस्त्र का निर्यात मुख्यतः हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों-ईरान, इराक, म्यांमार (बर्मा), श्रीलंका, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, मिस्र, सूडान, टर्की, इथोपिया, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि को करता है।
प्रश्न 9.
भारत में लौह-इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण, वितरण एवं भावी सम्भावनाओं का विवरण दीजिए। [2017]
या
भारत में लौह-इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कोई तीन कारण बताइए। [2013]
उत्तर :
भारत में लोहा-इस्पात उद्योग
उद्योग का महत्त्व एवं विकास
लोहा-इस्पात उद्योग की गणना भारत के महत्त्वपूर्ण भारी उद्योगों में की जाती है। वर्तमान में भारत में लोहा-इस्पात के 11 कारखाने है, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं। लोहा-इस्पात उद्योग, औद्योगिक क्रान्ति का जनक है। इस्पात का उपयोग मशीनों, रेलवे (UPBoardSolutions.com) लाइन, परिवहन के साधन, भवन निर्माण, रेल के पुल, जलयान, अस्त्र-शस्त्र तथा कृषि यन्त्र आदि बनाने में किया जाता है अर्थात् इससे एक सुई से लेकर विशालकाय टैंकों तक का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में भारत में एक इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) तथा शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

स्थानीयकरण के कारण – भारत में लोहा-इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
- लौह-अयस्क एवं कोयला जैसे कच्चे माल निकट स्थित होना।
- अन्य उपयोगी खनिज पदार्थों (मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट व चूना पत्थर) का मिलना।
- सस्ती एवं सुलभ जल विद्युत-शक्ति का मिलना।
- स्वच्छ जल की आपूर्ति होना
- विस्तृत उपभोक्ता बाजार की सुविधा प्राप्त होना।
- सस्ते एवं कुशल श्रमिकों का मिलना।
- परिवहन के सस्ते साधन का मिलना।
- पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था होना।
- उद्योग को सरकारी संरक्षण एवं सहायता प्राप्त होना।
उत्पादन एवं उद्योग के प्रमुख केन्द्र
भारत के प्रमुख लोहा-इस्पात कारखानों का विवरण निम्नलिखित है|
1. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर (TISCO) – इसे कम्पनी की स्थापना सन् 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा तत्कालीन बिहार (वर्तमान में झारखण्ड राज्य) के साँकची (वर्तमान में जमशेदपुर) नामक स्थान पर की गई थी। वर्तमान (UPBoardSolutions.com) में यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा-इस्पात कारखाना है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 20 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 19 लाख टन ढलवाँ लोहा प्रतिवर्ष तैयार करने की है। जमशेदपुर को ही इस्पात नगरी या टाटानगर भी कहा जाता है।
2. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (ISCO) – इस कम्पनी के अधीन इस्पात के तीन कारखाने-पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, कुल्टी तथा हीरापुर स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। सन् 1952 से इन तीनों कारखानों को ‘इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नाम से जाना जाता है। सन् 1976 से सरकार ने इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लिया है। बर्नपुर में इस्पात, हीरापुर में ढलवाँ लोहा तथा कुल्टी में इस्पात पिण्ड बनाए जाते हैं। इस कम्पनी का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इन तीनों इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन इस्पात तथा 13 लाख टन ढलवाँ लोहा तैयार करने की है।
3. विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड – कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर सन् 1923 में इस कारखाने की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र में पर्याप्त लौह-अयस्क निकाला जाता है, परन्तु कोयले का अभाव है। अत: कोयले के स्थान पर लकड़ी का कोयला प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ लौह-अयस्क केमानगुण्डी तथा बाबाबूदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 85,000 टन ढलवाँ लोहा तथा 2 लाख टन इस्पात तैयार करने की है। सन् 1962 ई० से इस कारखाने पर कर्नाटक सरकार तथा भारत सरकार का संयुक्त अधिकार है।

4. राउरकेला इस्पात लिमिटेड – ओडिशा राज्य में सन् 1955 में जर्मनी की सहायता से सुन्दरगढ़ जिले के राउरकेला नामक स्थान पर इस कारखाने की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 18 लाख टन इस्पात तैयार करने की है। इस कारखाने को (UPBoardSolutions.com) लौह-अयस्क क्योंझर तथा गुरुमहिसानी की खदानों से तथा कोयला झरिया, तालचेर एवं कोरबा की खदानों से प्राप्त होता है। हीराकुड बाँध से इसे , सस्ती जलविद्युत शक्ति प्राप्त होती है।
5. भिलाई इस्पात कारखाना – इस कारखाने की स्थापना वर्तमान छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर सन् 1955 ई० में तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार के सहयोग से की गई थी। इस कारखाने में उत्पादन सन् 1962 ई० में आरम्भ हुआ था। इस कारखाने को सभी भौगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष तैयार करने की है। यहाँ लोहे की छड़े, शहतीर, रेल की पटरियाँ तथा इस्पात के ढाँचे बनाए जाते हैं।
6. दुर्गापुर इस्पात कारखाना – पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार की सहायता से सन् 1956 ई० में इस कारखाने की स्थापना की गई थी परन्तु इस कारखाने से सन् 1962 ई० में उत्पादन प्रारम्भ हो सका। इसमें रेल की पटरियाँ, शहतीर तथा ब्लेड बनाए जाते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 16 लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करने की है।
7. बोकारो इस्पात कारखाना – वर्तमान झारखण्ड (तत्कालीन बिहार) राज्य के बोकारो नामक स्थान पर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् 1964 ई० में सोवियत संघ के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गई थी। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष तैयार करने की है।
अन्य प्रतिष्ठान – भारत में इस्पात की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए लोहा-इस्पात के अनेक नए कारखानों की स्थापना की गई है। इनमें कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जिले में हॉस्पेट के निकट विजयनगर, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में सलेम तथा ओडिशा राज्य में दैतारी नामक स्थानों पर नए इस्पात कारखानों की स्थापना प्रमुख है।
उत्पादन एवं व्यापार – भारत अनेक देशों को इस्पात का निर्यात करता है। न्यूजीलैण्ड, मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार (बर्मा), सऊदी अरब, श्रीलंका, कीनिया आदि देश भारतीय इस्पात के प्रमुख ग्राहक हैं। भविष्य में इस्पात के निर्यात की सम्भावना बढ़ी है।

लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
औद्योगिक ढाँचे का क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
भारत के औद्योगिक उद्यमों को मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कम्पनियाँ जिन पर सरकारी विभागों अथवा केन्द्र या राज्यों द्वारा स्थापित संस्थाओं का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। (UPBoardSolutions.com) दूसरे निजी क्षेत्र के उद्यम हैं। कुछ उद्यमों का मिश्रित रूप भी है जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था और निजी उद्यम दोनों का संयुक्त स्वामित्व होता है। संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों को कभी-कभी निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है
(क) गैर-कारखाना विनिर्माण इकाइयाँ – ये दो प्रकार की होती हैं
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग और
- अन्य औद्योगिक इकाइयाँ, जो इतनी छोटी होती हैं कि वे कारखाना कहलाने लायक नहीं होतीं और इसलिए उन्हें छोटी विनिर्माण इकाइयाँ कहा जाता है।
(ख) ऐसे उद्यम जिन्हें अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि भारत के लिए दुर्लभ स्रोत है। ये उद्यम विदेशी विनिमय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत काम करते हैं और फेरा (FERA) कम्पनियाँ कहलाते हैं। वर्तमान में ‘फेरा’ के स्थान पर ‘फेमा’ (FEMA) के नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है।
(ग) ऐसे उद्यम जो इतने बड़े हैं कि जिन्हें एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act) के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। इन्हें MRTP कम्पनियाँ कहते हैं। प्रश्न
प्रश्न 2.
पेट्रो-रसायन उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर :
पेट्रो-रसायन उद्योग रसायन उद्योग कम ही एक भाग है। इनके अन्तर्गत पेट्रोल, कोयला तथा अनेक रसायनों से विविध प्रकार के पदार्थ; जैसे—प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयाँ, रंग तथा रोगन आदि बनाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त पॉलीमर, कृत्रिम कार्बनिक रसायन, कृत्रिम रेशे तथा धागे, पॉलिस्टर, नाइलोन चिप्स, स्पेण्डेक्स धागे (तैराकी की पोशाकों हेतु) आदि भी बनाये जाते हैं। भारत में यह उद्योग स्वतन्त्रता के बाद आरम्भ किया गया। विगत दो दशकों में इसके उत्पादन तथा उपभोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकारी प्रोत्साहन तथा उदारीकरण ने इस उद्योग की प्रगति में विशेष योगदान दिया है।

प्लास्टिक प्रोसेसिंग मूलत: लघु उद्योग क्षेत्र में है। पेट्रो-रसायन उद्योग में बड़ी-बड़ी वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में इसका स्थान सर्वोपरि हो गया है। यह एक ऐसा उद्योग है, जिसमें कच्चे माल को पुनः परिष्कृत कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे इसकी महत्ता में और भी वृद्धि हो गयी है। पेट्रो-रसायन उद्योग मुम्बई के निकट ट्रॉम्बे एवं कोयली, गुजरात में अंकलेश्वर तथा बड़ोदरा में केन्द्रित हो गया है। इनके अतिरिक्त हल्दिया (प० बंगाल), डिगबोई (असोम), कोचीन (केरल), बरौनी (बिहार), चेन्नई (तमिलनाडु), करनाल (हरियाणा), मथुरा (उत्तर प्रदेश), (UPBoardSolutions.com) मार्मागाओ (गोवा) आदि स्थानों पर पेट्रो-रसायन उद्योग प्रगति पर है। इस उद्योग का प्रसार देश के अन्य भागों में भी होता जा रहा है। वर्ष 2004-05 में पेट्रो-रसायन पदार्थों का उत्पादन 7,018 किलो टन था। वर्ष 2009-10 में पेट्रो रसायन पदार्थों का उत्पादन 8.681 हजार मीट्रिक टन हो गया था।
प्रश्न 3.
पेट्रो-रसायन और रसायन उद्योग में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर :
पेट्रो-रसायन उद्योग खनिज तेल पर आधारित होते हैं। खनिज तेल को परिष्कृत करके उसमें से स्नेहक तेल, फर्नेस तेल, डीजल, मिट्टी का तेल, सफेद तेल, पेट्रोल, एल०पी०जी० गैस, नेफ्था, रासायनिक गोंद, ग्रीस, मेन्थॉल, नाइलोन, पॉलिस्टर प्राप्त किये जाते हैं। रेयॉन, नाइलोन, टेरीन और डेकरॉन कृत्रिम रेशे पेट्रो-रसायन उद्योग के वे उत्पाद हैं जिनसे आकर्षक, अधिक टिकाऊ वस्त्र बनाये जाते हैं। अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण पेट्रो-रसायन उत्पाद, परम्परागत कच्चे माल; जैसे-लकड़ी, शीशा और धातु का स्थान ले रहे हैं। घरों, कारखानों और खेतों में इनका उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए- प्लास्टिक के उपयोग से जन-जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। सिन्थेटिक डिटर्जेण्ट एक क्रान्तिकारी पेट्रो-रसायन उत्पाद ही है।
रसायन उद्योग – लोहा तथा इस्पात, इंजीनियारिंग और वस्त्र उद्योग के बाद रसायन उद्योग का देश में चौथा स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन उद्योग ने बड़ी तेजी से विकास किया है। ये उद्योग रसायनों पर आधारित होते हैं। इन भारी रसायनों से अनेक उत्पाद बनाये जाते हैं। इनमें औषधियाँ, रँगाई के सामान, नाशकमार (कीटनाशक आदि), पेण्ट, दियासलाई, साबुन आदि उत्पाद उल्लेखनीय हैं। अमेरिका का रसायन उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान है।
नाशकमार दवाओं में कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूदनाशक और कृतंकनाशक, कृषि और जन-स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। डी०डी०टी० बनाने का कारखाना सन् 1954 में दिल्ली में लगाया गया था। सन् 1996-97 में इसका उत्पादन १ 900 अरब मूल्य का था। औषध निर्माण उद्योग में भारत का अब विश्व में श्रेष्ठ स्थान है। देश मूलभूत तथा व्यापक (Bulk) औषधियों के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है।
प्रश्न 4.
सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अधिक केन्द्रित हैं, क्यों ? [2010]
उत्तर :
महाराष्ट्र के सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा एवं प्रमुख केन्द्र मुम्बई है। इस महानगर में सूती वस्त्रों की 71 मिले हैं, जिस कारण इसे ‘सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसी प्रकार अहमदाबाद गुजरात राज्य का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा एवं प्रमुख केन्द्र है। यहाँ सूती वस्त्रों की 81 मिले हैं, जिस कारण इसे भारत का मानचेस्टर’ तथा पूर्व का बोस्टन’ कहा जाता है। इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्रित होने के लिए (UPBoardSolutions.com) निम्नलिखित भौगोलिक कारण उत्तरदायी रहे हैं
1. कपास का पर्याप्त उत्पादन – महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की काली मिट्टी में कपास का पर्याप्त उत्पादन किया जाता है।
2. आर्द्र जलवायु – सागर की निकटता के कारण इन दोनों ही राज्यों की जलवायु आर्द्रता प्रधान है। इस जलवायु में बुनाई के समय धागा नहीं टूटता।
3. पत्तन की सुविधा मुम्बई तथा काँदला पत्तनों से सूती वस्त्र उद्योग हेतु मशीनें, कल-पुर्जे, रासायनिक पदार्थ, कपास तथा अन्य आवश्यक पदार्थों के विदेशों से आयात करने की सुविधा रहती
4. ऊर्जा के पर्याप्त साधन – इन केन्द्रों के सूती वस्त्र कारखानों को जलविद्युत शक्ति सस्ती दर पर सरलता से उपलब्ध हो जाती है।
5. पर्याप्त पूँजी – महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में पूँजीपति निवास करते हैं, जो बहुत ही धनाढ्य हैं; अर्थात् यहाँ इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है।
6. पर्याप्त माँग – यहाँ उत्पादित सूती वस्त्रों का उपभोक्ता बाजार बड़ा ही विस्तृत है।
7. सस्ते एवं कुशल श्रमिक – मुम्बई तथा अहमदाबाद महानगरों में परम्परागत, सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

प्रश्न 5.
हुगली नदी के किनारे कागज के अनेक कारखाने क्यों स्थापित हो गये हैं ?
उत्तर :
पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे कागज के अनेक कारखाने स्थापित हुए हैं। यहाँ इस उद्योग की स्थापना के निम्नलिखित कारण हैं
- पश्चिम बंगाल तथा उसके समीपवर्ती राज्यों में घास पर्याप्त मात्रा में उगती है, जो कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यहाँ उत्पादित बॉस का उपयोग भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- कागज उद्योग में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। हुगली नदी के सदावाहिनी होने के कारण यहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। यही एक प्रमुख कारण है कि हुगली नदी के किनारे टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, आलम बाजार, कोलकाता, बाँसबेरिया तथा शिवराफूली में कागज के कारखाने स्थापित किये गये हैं।
- कागज उद्योग के लिए आवश्यक शक्ति-संसाधन पश्चिम बंगाल (UPBoardSolutions.com) राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
- पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्यों में पर्याप्त संख्या में कुशल एवं अनुभवी श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं।
- कागज उद्योग के विकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है, जिससे कच्चा माल आयात करने तथा तैयार माल देश के विभिन्न भागों में भेजने की सुविधा रहती है।
प्रश्न 6.
भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं
- देश में उत्तम कपास की कमी है। देश के विभाजन के कारण अच्छी कपास उत्पन्न करने वाले दो क्षेत्र (पंजाब का पश्चिमी भाग तथा सिन्ध) पाकिस्तान में चले गये।
- इस उद्योग को जापान, चीन, पाकिस्तान आदि देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों में लम्बे रेशे की कपास सुलभ होने तथा आधुनिक मशीनों एवं विधियों के प्रयोग के कारण उत्पादन लागत बहुत कम है।
- सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मशीनें घिसी हुई तथा पुरानी हैं, जिस कारण देश में वस्त्र की उत्पादन लागत अधिक आती है।
- अनेक मिलें अनार्थिक आकार की हैं, जिस कारण इन्हें आन्तरिक किफ़ायत प्राप्त नहीं हो पाती। फलतः उत्पादन-लागत बढ़ जाती है।
- सूती वस्त्रों पर सरकार द्वारा आरोपित उत्पादन कर अधिक है।

प्रश्न 7.
भारत में लौह-इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठार के आस-पास क्यों केन्द्रित है? दो प्रमुख कारणों का उल्लेख, कीजिए।
उतर :
लोहा-इस्पात उद्योग की दो आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं-लौह-अयस्क तथा कोयला। छोटा नागपुर का पठार इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार करता है। यही कारण है कि लौह-इस्पात उद्योग इसके आस-पास ही केन्द्रित हैं। दोनों कारणों का संक्षिप्त उल्लेख आगे किया जा रहा है
- लौह-अयस्क की उपलब्धता – भारत के कुल लौह-अयस्क उत्पादन का 40% लौह-अयस्क छोटा नागपुर की खानों से निकाला जाता है। यहाँ लौह-खनिज के लिए सिंहभूम जिला महत्त्व रखता है। सिंहभूम और ओडिशा की सीमा (UPBoardSolutions.com) पर कोल्हन पहाड़ियाँ लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- कोयला – भारत का 90% कोकिंग कोयला झरिया की खानों से मिलता है। भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ 2,000 लाख टन कोयले के भण्डार हैं। यह कोयला यहाँ के आस-पास स्थित लोहा-इस्पात के उद्योगों को सरलता से बिना अधिक परिवहन व्यय के उपलब्ध है।
उपर्युक्त दो कारणों से अधिकांश लोहा-इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठार के आस-पास ही स्थित हैं, जिनमें टाटा लोहा-इस्पात कारखाना, जमशेदपुर, बोकारो स्टील प्लाण्ट, दुर्गापुर इस्पात कारखाना आदि मुख्य हैं।
प्रश्न 8.
आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? इनका क्या महत्त्व है? [2009]
उत्तर
लोहा-इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा-इस्पात उद्योग की गणना भारत के महत्त्वपूर्ण भारी उद्योगों में की जाती है। वर्तमान समय में भारत में लोहा-इस्पात के 11 कारखाने हैं। लोहा-इस्पात उद्योग औद्योगिक क्रान्ति का जनक है। इस्पात का उपयोग मशीनों, रेलवे लाइन, परिवहन के साधन, भवन-निर्माण, रेल के पुल, जलयान, अस्त्र-शस्त्र तथा कृषि-यन्त्र आदि के निर्माण में किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में एक इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) तथा शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
लौह-इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है ?
उत्तर :
लोहा और इस्पात से भारी मशीनें तथा औजार बनाये जाते हैं। यही मशीनें तथा औजार अन्य उद्योगों के आधार हैं। यही कारण है कि लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है।
प्रश्न 2 भारत में प्रथम आधुनिक इस्पात कारखाना कहाँ तथा कब स्थापित किया गया ?
उत्तर भारत में प्रथम आधुनिक इस्पात कारखाना 1907 ई० (UPBoardSolutions.com) में जमशेदपुर में (वर्तमान में झारखण्ड राज्य के साँकची नामक स्थान) लगाया गया।
प्रश्न 3.
लौह-इस्पात उद्योग के चार प्रमुख केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
लोहा-इस्पात उद्योग के चार प्रमुख केन्द्रों के नाम हैं—
- भिलाई,
- बोकारो,
- जमशेदपुर तथा
- राउरकेला।
प्रश्न 4.
चीनी उद्योग के प्रमुख केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
चीनी उद्योग के प्रमुख केन्द्र अर्थात् चीनी उत्पादक प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं
- महाराष्ट्र,
- उत्तर प्रदेश,
- कर्नाटक,
- तमिलनाडु,
- बिहार,
- आन्ध्र प्रदेश आदि।

प्रश्न 5.
भारत में सूती वस्त्रोद्योग किन राज्यों में महत्वपूर्ण है ? कुछ प्रमुख केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
भारत के गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में सूती वस्त्रोद्योग (UPBoardSolutions.com) महत्त्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख केन्द्र मुम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, कानपुर आदि हैं।
प्रश्न 6.
भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र लिखिए।
उत्तर :
अमृतसर, लुधियाना, मुम्बई, कानपुर, जामनगर, श्रीनगर आदि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं।
प्रश्न 7.
भारत के तीन राज्यों के नाम बताइए, जहाँ रेशम अधिक पैदा होता है।
या
भारत में रेशमी वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केन्द्र बताइए।
उत्तर :
भारत के वे राज्य; जहाँ रेशम अधिक पैदा होता है; के नाम हैं—
- कर्नाटक,
- तमिलनाडु,
- आन्ध्र प्रदेश,
- असोम आदि।
प्रश्न 8.
भारत में अखबारी कागज का प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया ?
उत्तर :
भारत में अखबारी कागज का प्रथम कारखाना सन् 1955 ई० में नेपानगर (म० प्र०) में स्थापित किया गया।
प्रश्न 9 .
लेम किसलिए प्रसिद्ध है ?
उत्तर :
सलेम इस्पात संयन्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
प्रश्न 10.
बड़ोदरा कहाँ स्थित है ? यह किसलिए प्रसिद्ध है ?
उत्तर :
ड़ोदरा गुजरात राज्य में स्थित है। यह सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्र, सीमेण्ट उद्योग तथा पेट्रो-रसायन के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न 11.
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के तीन केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
- बंगलुरु (कर्नाटक),
- हैदराबाद (तेलंगाना) तथा
- पिंजौर (हरियाणा), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के तीन केन्द्र हैं।

प्रश्न 12.
लोकोमोटिव उद्योग के दो केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
- चितरंजन (प० बंगाल) तथा
- वाराणसी (उत्तर प्रदेश), लोकोमोटिव उद्योग के दो प्रधान केन्द्र हैं।
प्रश्न 13.
पोत (जलयान) निर्माण के चार केन्द्र कौन-कौन से हैं ?
उत्तर :
- मझगाँव डॉक, मुम्बई,
- कोचीन शिपयार्ड, केरल,
- गार्डन रीच, कोलकाता तथा
- विशाखापत्तनम् पोत-निर्माण के चार केन्द्र हैं।
प्रश्न 14.
भिलाई किस उद्योग से सम्बन्धित है ?
उत्तर :
भिलाई लोहा-इस्पात उद्योग से सम्बन्धित है।
प्रश्न 15.
नेपानगर किस प्रदेश में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है ?
उत्तर :
नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

प्रश्न 16.
विशाखापत्तनम् किस उद्योग से सम्बन्धित है ?
उत्तर :
विशाखापत्तनम् लोहा-इस्पात उद्योग (UPBoardSolutions.com) और जहाज-निर्माण उद्योग से सम्बन्धित है।
प्रश्न 17.
जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है ?
उत्तर :
जमशेदपुर झारखण्ड राज्य में स्थित है।
प्रश्न 18.
कृषि उत्पादों पर आधारित किन्हीं चार उद्योगों के नाम लिखिए। [2010, 14]
उत्तर :
कृषि उत्पादों पर आधारित चार उद्योगों के नाम हैं–
- सूती वस्त्र उद्योग,
- चीनी उद्योग,
- जूट उद्योग तथा
- चाय उद्योग।
प्रश्न 19.
भारत में कागज उद्योग के दो प्रमुख केन्द्रों के नाम लिखिए।
उत्तर :
भारत में कागज उद्योग के दो प्रमुख केन्द्र हैं-मध्य प्रदेश में अमलाई तथा महाराष्ट्र में बल्लारपुर।
प्रश्न 20.
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के एक-एक लौह-इस्पात कारखाने का नाम लिखिए।
उत्तर :
सार्वजनिक क्षेत्र – दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।
निजी क्षेत्र – टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, झारखण्ड।
प्रश्न 21.
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों के नाम लिखिए।
उत्तर :
- भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई, छत्तीसगढ़ तथा
- बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो, (UPBoardSolutions.com) झारखण्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के दो इस्पात कारखाने हैं।
प्रश्न 22.
भारत के पेट्रो-रसायन के किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए।
उत्तर :
- प्लास्टिक उद्योग तथा
- सिन्थेटिक डिटर्जेण्ट उद्योग; पेट्रो-रसायन के दो उद्योग हैं।

प्रश्न 23.
भारत में कौन-सा नगर ‘सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है ?
उत्तर :
महाराष्ट्र के मुम्बई नगर को ‘सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है।
प्रश्न 24.
भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण किन दो स्थानों पर होता है ?
उत्तर :
भारत में रेल के डिब्बों का निर्माण–
- पेराम्बुर (चेन्नई के निकट) तथा
- कपूरथला, पंजाब नामक दो स्थानों पर होता है।
प्रश्न 25.
भारत में औद्योगिक दृष्टि से विकसित दो राज्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
महाराष्ट्र तथा गुजरात।
प्रश्न 26.
टाटा आयरन स्टील कम्पनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ? [2015]
उत्तर :
टाटा आयरन स्टील कम्पनी का मुख्यालय जमशेदपुर में है।
प्रश्न 27.
सीमेण्ट के निर्माण में किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है ?
उत्तर :
सीमेण्ट के निर्माण में चूना-पत्थर का (UPBoardSolutions.com) उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 28 .
पेट्रो-रसायन उद्योग का सम्बन्ध किस खनिज पदार्थ से है ?
उत्तर :
पेट्रो-रसायन उद्योग का सम्बन्ध गैस, एल्कोहल, कैल्सियम, लकड़ी, शशा और धात्विक खनिजों से है।
प्रश्न 29.
चीनी उद्योग की प्रमुख चार समस्याएँ लिखिए।
उत्तर :
भारत में चीनी उद्योग की चार प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं.
- उत्तम किस्म के गन्ने की कमी होना।
- चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का आंशिक भाग ही प्रयुक्त कर पाना।
- उत्पादन लागतों में लगातार वृद्धि होना।
- मिलों में आधुनिक तकनीकी तथा मशीनों के प्रयोग का अभाव होना।

प्रश्न 30.
कुटीर उद्योग की दो समस्याओं को लिखिए।
उत्तर :
कुटीर उद्योग की दो समस्याएँ निम्नलिखित हैं
- बैंकों से ऋण मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इन्हें मजबूर होकर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है।
- इन उद्योगों को चलाने के लिए कुशल (UPBoardSolutions.com) प्रबन्धक नहीं मिल पाते।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. लोहा-इस्पात उद्योग कहाँ संकेन्द्रित हैं?
(क) गंगा घाटी में ,
(ख) दामोदर घाटी में
(ग) दकन के पठार में
(घ) बिहार में
2. रेलवे कोच बनाये जाते हैं
(क) पटियाला में
(ख) मेरठ में
(ग) कपूरथला में
(घ) येलाहांका में
3. नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से सम्बन्धित है? [2015]
(क) कागज उद्योग
(ख) चीनी उद्योग
(ग) सीमेण्ट उद्योग
(घ) लोहा तथा इस्पात उद्योग
4. ‘प्लास्टिक’ किस उद्योग का प्रमुख उत्पाद है?
(क) रसायन
(ख) पेट्रो-रसायन,
(ग) सिन्थेटिक वस्त्र
(घ) उर्वरक
5. भारत में कागज का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
(क) कुल्टी में
(ख) नेपानगर में
(ग) टीटागढ़ में
(घ) सिरामपुर में

6. निम्नलिखित में से कौन-सा नगर कागज उद्योग से सम्बन्धित है? [2013, 15, 17] “
(क) कानपुर
(ख) नेपानगर
(ग) जयपुर
(घ) लखनऊ
7. पेट्रो-रसायन उद्योग का प्रमुख केन्द्र है
(क) बड़ोदरा
(ख) अहमदाबाद
(ग) बंगलुरु
(घ) कानपुर
8. भारत में सबसे अधिक सीमेण्ट कारखाने किस राज्य में हैं?
(क) मध्य प्रदेश में ,
(ख) उत्तर प्रदेश में
(ग) आन्ध्र प्रदेश में
(घ) बिहार में
9. किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं?
(क) बिहार में
(ख) उत्तर प्रदेश में
(ग) महाराष्ट्र में।
(घ) मध्य प्रदेश में

10. निम्नलिखित में कौन-सा उद्योग कृषि पर आधारित है?
(क) सीमेण्ट उद्योग
(ख) सूती वस्त्र उद्योग
(ग) इस्पात उद्योग
(घ) रसायन उद्योग
11. ‘भारत का मैनचेस्टर’ और ‘पूर्व का बोस्टन’ कहलाता है [2012, 14]
(क) कानपुर
(ख) मुम्बई
(ग) अहमदाबाद
(घ) जमशेदपुर
12. निम्नलिखित में से कागज उद्योग से कौन-सा स्थान सम्बन्धित है? (2012)
(क) आगरा।
(ख) फिरोजाबाद
(ग) टीटागढ़
(घ) धनबाद

13. निम्नलिखित में से कौन-सा नगर सीमेण्ट उद्योग से सम्बन्धित है? [2013]
(क) कटनी
(ख) आगरा।
(ग) भोपाल
(घ) ग्वालियर
14. निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? [2013, 15]
(क) सूती वस्त्र उद्योग
(ख) चीनी उद्योग
(ग) सीमेण्ट उद्योग
(घ) जूट उद्योग
15. उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? [2014]
(क) लुधियाना
(ख) दिल्ली
(ग) कानपुर
(घ) लखनऊ
16. निम्न में से किसे इस्पात-नगरी कहा जाता है? [2014, 16]
(क) भिलाई
(ख) बोकारो
(ग) जमशेदपुर
(घ) राउरकेला
17. राउरकेला लोहा-इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? [2014]
(क) बिहार
(ख) छत्तीसगढ़
(ग) ओडिशा
(घ) उत्तर
प्रदेश 18. भिलाई सम्बन्धित है [2015]
(क) सीमेण्ट उद्योग से
(ख) लौह-इस्पात उद्योग से
(ग) जूट उद्योग से
(घ) ऐलुमिनियम उद्योग से
19. किसी उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? [2015]
(क) कच्चा माल
(ख) जल
(ग) परिवहन
(घ) उपर्युक्त सभी

20. भिलाई लौह-इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? [2017]
(क) बिहार
(ख) छत्तीसगढ़
(ग) ओडिशा
(घ) उत्तर प्रदेश
21. निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह-इस्पात संयन्त्र स्थापित है? [2017, 18]
(क) मध्य प्रदेश
(ख) बिहार
(ग) झारखण्ड
(घ) छत्तीसगढ़
उत्तरमाला
1. (ख), 2. (ग), 3. (क), 4. (ख), 5. (घ), 6. (ख), 7. (क), 8. (क), 9. (ग), 10. (ख), 11. (ग), 12. (ग), 13. (क), 14. (ग), 15. (ग), 16. (ग), 17.(ग), 18. (ख), 19. (घ), 20. (ख), 21. (ग)।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 मानवीय संसाधन : विनिर्माणी उद्योग (अनुभाग – तीन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 11 मानवीय संसाधन : विनिर्माणी उद्योग (अनुभाग – तीन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()