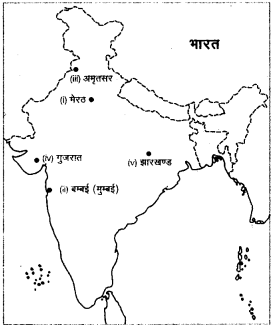UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 22 Mental Health and Mental Hygiene (मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान) are part of UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 22 Mental Health and Mental Hygiene (मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान).
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Pedagogy |
| Chapter |
Chapter 22 |
| Chapter Name |
Mental Health and Mental Hygiene
(मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान) |
| Number of Questions Solved |
55 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 22 Mental Health and Mental Hygiene (मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
मानसिक स्वास्थ्य से क्या आशय है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
या
मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी क्यों होनी चाहिए? [2010, 11, 13]
या
मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी क्यों आवश्यक है? [2011]
या
मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (2016)
या
मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? (2015)
या
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (2015)
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ
मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके माध्यम से वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर हर परिस्थिति में अपने को समायोजित कर लेता है। सुखी जीवन के लिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी। चिकित्साशास्त्रियों के अनुसार, सामान्य शारीरिक व्याधियाँ; जैसे-रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि मानसिक कारकों से उत्पन्न होती हैं।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति चिन्तारहित, पूर्णतः समायोजित, आत्मनियन्त्रित, आत्मविश्वासी तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है। उसके व्यवहार में सन्तुलन रहता है तथा वह अधिक समय तक मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं रहता। वह प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को शीघ्र ही समायोजित कर लेता है। वर्तमान परिस्थितियों में, सम्पूर्ण समाज में, उसके विभिन्न अंगों में तथा उसके नागरिकों के बीच अच्छे-से-अच्छा समायोजन व्यापक कल्याण का द्योतक है जिसके लिए मानसिक स्वास्थ्य एक पूर्ण आवश्यकता है।
मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा
विभिन्न विद्वानों ने मानसिक स्वास्थ्य की अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।
- हैडफील्ड के अनुसार, “साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है।”
- लैडेल के मतानुसार, “मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है–वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता।”
- प्रो० भाटिया के शब्दों में, “मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की माँगों और अंवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह समायोजित है।”
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण
जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य की भी कुछ लक्षणों के आधार पर पहचान सम्भव है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य एक कल्पना मात्र है और कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता, तथापि मानसिक स्वास्थ्य से सम्पन्न व्यक्ति के कुछ विशिष्ट लक्षण अवश्य हैं। इनमें सर्वप्रथम हैडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की नितान्त आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा और इसके बाद अन्य प्रमुख लक्षणों का विवेचन किया जाएगा। ये निम्न प्रकार हैं।
1.पूर्ण :
अभिव्यक्ति पर निर्भर है। इसके अवद्मन से वृत्तियाँ दमित वे कुण्ठित होकर व्यक्तित्व में मानसिक विकारों तथा कुसमायोजन का कारण बनती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
2. सन्तुलन :
व्यक्ति को भावना ग्रन्थियों के निर्माण, प्रतिरोध व मानसिक द्वन्द्व जैसे दोषों से बचाने के लिए आवश्यक है कि उसकी मूल-प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा समस्त क्षमताओं के बीच आपसी सन्तुलन व वातावरण से समायोजन बना रहे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सन्तुलन और समायोजन परमावश्यक है।
3. सामान्य लक्षण :
विभिन्नताओं, क्षमताओं, इच्छाओं वे प्रवृत्तियों के बीच सन्तुलन व समन्वय तथा उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति सिर्फ तभी सम्भव है, जब वे एक सामान्य एवं
व्यापक लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। ये लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्धारित किये जाने चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से सम्बन्धित है जिसके लिए व्यक्तित्व के गुणों की पूर्ण अभिव्यक्ति, उनकी सन्तुलित क्रियाशीलता तथा सामान्य एवं व्यापक लक्ष्य आवश्यक हैं।
I. अन्य प्रमुख लक्षण
मानसिक स्वास्थ्य को कुछ अन्य प्रमुख लक्षणों के आधार पर भी पहचाना जाता है, जो अग्र प्रकार वर्णित हैं।
1. अन्तर्दृष्टि एवं आत्म-मूल्यांकन :
जिस व्यक्ति में स्वयं के समायोजन सम्बन्धी समस्याओं की अन्तर्दृष्टि होती है, वह अपनी सामर्थ्य की अधिकतम और निम्नतम दोनों सीमाओं से भली-भाँति परिचित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर या तो उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है या उनसे
समझौता कर लेता है। वह आत्म-दर्शन तथा आत्म-विश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी उलझनों, तनावों, पूर्वाग्रहों, अन्तर्द्वन्द्वों तथा विषमताओं का सहज समाधान खोजकर उन्हें समाप्त या कम करने की कोशिश करना है। वह अपनी इच्छाओं, क्षमताओं तथा शक्तियों का वास्तविक मूल्यांकन करके उन्हें सही दिशा प्रदान पर सकता है।
2. समायोजनशीलता :
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लचीलेपन के गुण के कारण नवीन एवं परिवर्तित परिस्थितियों से शीघ्र एवं उचित समायोजन स्थापित करने में सफल रहता है। वह विषम परिस्थितियों से भय खाकर या घबराकर उनसे पलायन नहीं करता, अपितु उनको दृढ़ता से सामना करती है और उनके बीच से ही अपना मार्ग खोज लेता है। समायोजनशीलता के अन्तर्गत दोनों ही बातें सम्मिलित हैं
- परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना या
- स्वयं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। स्वस्थ व्यक्ति समाज के परिवर्तनशील नियमों तथा रीति-रिवाजों से परिचित होने के कारण उनसे उचित सामंजस्य स्थापित कर लेता है।
3. बौद्धिक तथा सांवेगिक परिपक्वता :
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बौद्धिक एवं सांवेगिक परिपक्वता की नितान्त आवश्यकता है। बौद्धिक परिपक्वता से युक्त मनुष्य अपने ज्ञान का विस्तार करता है, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है तथा अपना निर्माण स्वयं करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रखर बुद्धि से अहम् भाव तथा मन्द बुद्धि से हीनमन्यता का जन्म हो सकता है। अतः बौद्धिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके प्रति सतर्कता आवश्यक है। सांवेगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने संवेगों तथा भावों पर उचित नियन्त्रण रखता है। वह सांवेगिक ग्रन्थियों (यथा-ईष्र्या, उन्माद आदि) से पूर्णतया मुक्त होता है। स्पष्टतः मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति में बौद्धिक एवं सांवेगिक परिपक्वता आवश्यक है।
4. यथार्थदृष्टिकोण एवं स्वस्थ अभिवृत्ति :
मानसिक स्वास्थ्य से युक्त व्यक्ति जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण तथा स्वस्थ अभिवृत्ति अपनाता है। ऐसे व्यक्ति के विचारों, वृत्तियों, आकांक्षाओं तथा कार्य-पद्धति के बीच उचित सन्तुलन रहने से वह कल्पना प्रधान, अतिशयवादी या कोरा स्वप्नदृष्टा नहीं – होता। वह उच्च एवं हीन भावना ग्रन्थियों के विकार से मुक्त होकर स्वविवेक के आधार पर कार्य करता है। उसकी प्रवृत्तियों तथा अभिवृत्तियों के बीच विरोधाभास दिखायी नहीं देता। वह जो कुछ है उसका यथार्थ मूल्यांकन कृरता है और तद्नुसार ही कार्य में रत हो जाता है। उसकी कथनी-करनी में भेद नहीं रहता। इस प्रकार वह अपने जीवन के विषय में वास्तविक दृष्टि एवं श्रेष्ठ अभिवृत्तियाँ अपनाकर सन्तुलित एवं संयमित जीवन व्यतीत करता है।
5. व्यावसायिक सन्तुष्टि :
मानसिक स्वास्थ्य की एक प्रमुख विशेषता अपने व्यवसाय अथवा कार्य के प्रति पूर्ण सन्तुष्टि की अनुभूति भी है। अपने कार्य से सन्तुष्ट व्यक्ति मन लगाकर कार्य करता है और श्रम से पीछे नहीं हटता। उसकी कार्यक्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के प्रति सुनिश्चित एवं दृढ़ बनाती है। परिणामतः वह व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर श्रीसम्पन्न जीवन बिताता है। इसके विरुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से असन्तुष्ट व्यक्ति आर्थिक विपन्नता, निराशा, चिन्ता तथा तनावों से ग्रस्त रहते हैं। वे मानसिक रोगी हो जाते हैं।
6. सामाजिक सामंजस्य :
व्यक्ति अपने समाज का एक अविभाज्य अंग है और उसकी एक इकाई है। उसकी अपूर्ण सत्ता समाज की पूर्णता में समाहित होकर परिपूर्ण होती है। अत: उसका समाज के साथ समायोजन, अनुकूलन तथा संमन्वय सर्वथा प्राकृतिक एवं अनिवार्य कहा जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के साथ सामंजस्य बनाकर रखता है। वह हमेशा समाज की समस्याओं और मर्यादाओं का ध्यान रखता है।
वह केवल अपने सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही प्रचेष्ट नहीं रहता, अपितु समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करता है। वह स्व-हित और पर-हित के मध्य सन्तुलन बनाकर चलता है। समाज के साथ प्रतिकूल एवं तनावपूर्ण सम्बन्ध मानसिक अस्वस्थता के परिचायक हैं। उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नियमित जीवन बिताने वाले आत्मविश्वासी, सहनशील, धैर्यवान एवं सन्तोषी मनुष्य होते हैं। उनकी इच्छाएँ तथा आवश्यकताएँ सामाजिक मान्यताओं की सीमाओं में और उसकी आदतें समाज के लिए हितकर होती हैं।
प्रश्न 2
मानसिक अस्वस्थता से आप क्या समझते हैं ? मानसिक अस्वस्थता के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए।
या
दो प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवरण दीजिए जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। [2017,2010]
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता का आशय
जब कोई मनुष्य अपने कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में असमर्थ रहता है, अथवा उने बाधाओं से उचित समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तो उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है और उसमें मानसिक-अस्वस्थता’ पैदा हो जाती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति स्वयं को अपने वातावरण की परिस्थितियों के साथ समायोजित न करने के कारण सांवेगिक दृष्टि से अस्थिर हो जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, मानसिक उलझनों, तनावों, हताशा व चिन्ताओं के कारण उसमें भाव-ग्रन्थियाँ बन जाती हैं तथा वह व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेकानेक अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाता है।
इस प्रकार से, मानसिक अस्वस्थता वह स्थिति है जिसमें जीवन की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में व्यक्ति स्वयं को असमर्थ पाता है तथा संवेगात्मक असन्तुलन का शिकार हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में बहुत-सी मानसिक विकृतियाँ या व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाता है।”
मानसिक अस्वस्थता के लक्षण
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में उन सभी लक्षणों का अभाव रहता है जिनका मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के रूप में अध्ययन किया गया है। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार से लेकर उसके पागलपन की स्थिति के बीच में अनेकानेक स्तर या सोपान दृष्टिगोचर होते हैं, तथापि मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख लक्षणों का सोदाहरण, किन्तु संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है
1. साधारण समायोजन सम्बन्धी दोष :
साधारण समायोजन सम्बन्धी दोष के लक्षण प्राय: प्रत्येक व्यक्ति में पाये जाते हैं। इसे मानसिक अस्वस्थता का एक सामान्य रूप कहा जा सकता है। अक्सर देखने में आता है कि कोई बावा या अवरोध उत्पन्न होने के कारण अपने कार्य की सम्पन्नता में असफल रहने वाला व्यक्ति अति संवेदनशील, हठी, चिड़चिड़ा या आक्रामक हो जाता है। यह मानसिक अस्वस्थता की शुरुआत है।
2. मनोरुग्णता :
सामान्य जीवन वाले कुछ लोगों में भी मानसिक अस्वस्थता के संकेत दिखाई पड़ते हैं। लिखने-पढ़ने, बोलने या अन्य क्रियाकलापों में अक्सर लोगों से भूल होना स्वाभाविक ही है। और इसे मानसिक अस्वस्थता का नाम नहीं दिया जा सकता, किन्तु यदि इन भूलों की आवृत्ति बढ़ जाए और असामान्य-सी प्रतीत हो तो इसे मनोविकृति कहा जाएगा। तुतलाना, हकलाना, क्रम बिगाड़ कर वाक्य बोलना, बेढंगे तथा अप्रचलित वस्त्र धारण करना, चलने-फिरने में असामान्य लगना, अजीब-अजीब हरकतें करना, चोरी करना, धोखा देना आदि मानसिक अस्वस्थता के लक्षण हैं।
3. मनोदैहिक रोग :
मनोदैहिक रोगों का कारण व्यक्ति के शरीर में निहित होता है। उदाहरण के लिए-शरीर के किसी संवेदनशील भाग में चोट या आघात के कारण स्थायी दोष पैदा हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवनभर कष्ट देते हैं। सिगरेट, तम्बाकू, अफीम, चरस, गाँजा या शराब आदि पीने से भी अनेक मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। दमा-खाँसी से चिड़चिड़ापन, निम्न या उच्च रक्तचाप के कारण मानसिक असन्तुलन तथा यकृत एवं पाचन सम्बन्धी व्याधियों से बहुत-से मानसिक विकारों का जन्म होता है। इसी के साथ-साथ किसी प्रवृत्ति का बलपूर्वक दमन करने से रक्त की संरचना, साँस की प्रक्रिया तथा हृदय की धड़कनों में परिवर्तन आता है, जिसके परिणामत: व्यक्ति का शरीर हमेशा के लिए रोगी हो जाता है। इस प्रकार शरीर और मन दोनों ही मानसिक अस्वस्थता से प्रभावित होते हैं।
4. मनस्ताप :
मनस्ताप (Psychoneuroses) का जन्म समायोजन-दोषों की गम्भीरता के परिणामस्वरूप होता है। ये व्यक्तित्व के ऐसे आंशिक दोष हैं जिनमें यथार्थता से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो पाता। इसमें
- स्नायु दौर्बल्य तथा
- मनोदौर्बल्य रोग सम्मिलित हैं।
1. स्नायु दौर्बल्य
इसमें व्यक्ति अकारण ही थकावट अनुभव करता है। इससे उसमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, विभिन्न अंगों में दर्द, काम के प्रति अनिच्छा, मंदाग्नि, दिल धड़कना तथा हमेशा अपने स्वास्थ्य की चिन्ता के लक्षण दिखायी पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी एक डॉक्टर के पास नहीं टिकता और अपनी व्यथा कहने के लिए बेचैन रहता है।
2. मनोदौर्बल्य
मनोदौर्बल्य में निम्नलिखित मानसिक विकार आते हैं
- कल्पना गृह या विश्वासबाध्यता के रोगी के मन में निराधार वे असंगत विचार, विश्वास और कल्पनाएँ आती रहती हैं।
- हठप्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति कामों की निरर्थकता से परिचित होते हुए भी उन्हें हठपूर्वक करता : रहता है और बाद में दु:ख भी पाता है।।
- भीतियाँ के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष प्रकार की चीजों, दृश्यों तथा विचारों से अकारण ही भयभीत रहता है; जैसे-खुली हवा से डरना, भीड़, पानी आदि से डरना।
- शरीरोन्माद में व्यक्ति के अहम् द्वारा दमित कामवासनाओं को शारीरिक दोषों के रूप में प्रकटीकरण होना; जैसे-हँसना, रोना, हाथ-पैर पटकना, मांसपेशियों का जकड़ना, मूच्छ आदि।
- चिन्ता रोग में अकारण ही भविष्य सम्बन्धी चिन्ताएँ लगी रहती हैं।
- क्षति क्रमबाध्यता से ग्रस्त व्यक्ति अकारण ही ऐसे काम कर बैठता है जिससे अन्य व्यक्तियों को, हानि हो; जैसे—मारना-पीटना, हत्या या दूसरे के घर में आग लगा देना। इस रोग का सबसे अच्छा उदाहरण ‘कनपटीमार व्यक्ति का आतंक है जो कनपटी पर मारकर अकारण ही लोगों की हत्या कर देता था।
5. मनोविकृतिये :
गम्भीर मानसिक रोग हैं, जिनके उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय में दाखिल होना पड़ता है। मनोविकृति से पीड़ित व्यक्तियों का यथार्थ से पूरी तरह सम्बन्ध टूट जाता है। वे अनेक प्रकार के भ्रमों व भ्रान्तियों के शिकार हो जाते हैं और उन्हें सत्य समझने लगते हैं। मनोविकृति के अन्तर्गत ये रोग आते हैं—स्थिर भ्रम (Parangia) से ग्रसित किसी व्यक्ति को पीड़ा भ्रम (Delusions ofPersecution) रहने के कारण वह स्वयं को पीड़िते समझ बैठता है, तो किसी व्यक्ति में ऐश्वर्य भ्रम (Delusion of Prosperity) पैदा होने के कारण वह स्वयं को ऐश्वर्यशाली या महान् समझता है। उत्साह-विषाद चक्र, मनोदशा (Manic Depressive Psychosis) का रोगी कभी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ता है तो कभी उदास।
6. यौन विकृतियाँ :
मानसिक रोगी का यौन सम्बन्धी या लैंगिक जीवन सामान्य नहीं होता। यौन विकृतियाँ मानसिक अस्वस्थता की परिचायक हैं और अस्वस्थता में वृद्धि करती हैं। इनके प्रमुख लक्षण ये हैं–विपरीत लिंग के वस्त्र पहनना, स्पर्श से यौन सुख प्राप्त करना, स्वयं को या दूसरे को पीड़ा पहुँचाकर काम सुख प्राप्त करना, बालकों, पशुओं, समलिगियों तथा शव से यौन क्रियाएँ करना, हस्तमैथुन तथा गुदामैथुन आदि।
उपर्युक्त वर्णित विभिन्न मनोरोगों का उनके सम्बन्धित लक्षणों के साथ वर्णन किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति में ये सभी लक्षण दिखायी पड़े, इनमें से कोई एक लक्षण भी मानसिक अस्वस्थता का संकेत देता है। व्यक्ति में इन लक्षणों के प्रकट होते ही उसका मानसिक उपचार किया जाना चाहिए।
प्रश्न 3
मानसिक अस्वस्थता के कारणों अथवा मानसिक स्वास्थ्य में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए।
या
मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में बाधा डालने वाले तत्त्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ एवं परिभाषा के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखें। मानसिक अस्वस्थता के कारण
अथवा
मानसिक स्वास्थ्य में बाधक कारक मानसिक अस्वस्थता के कारण ही वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य में बाधक कारक होते हैं। इस वर्ग के मुख्य कारकों का विवरण निम्नलिखित है
1. शारीरिक कारण :
कभी-कभी मानसिक अस्वस्थता के मूल में शारीरिक कारण निहित होते हैं। प्रायः क्षय, संग्रहणी, कैंसर आदि असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की शारीरिक शक्ति काफी घट जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शीघ्र ही थकान का अनुभव होने लगता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़े और दुःखी होते हैं, क्योंकि उनमें जीवन के प्रति निराशा छा जाती है।
2. वंशानुगत देन :
कुछ मनुष्य वंशानुक्रम से ऐसी विशेषताएं लेकर उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से वे सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। वंशानुक्रमणीय विशेषताओं के कारण ही मनोविकृति का रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होता रहता है।
3. संवेगात्मक कारण :
मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग मानसिक रोगों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। व्यक्ति की। विभिन्न मूल-प्रवृत्तियाँ किसी-न-किसी संवेग से सम्बन्धित हैं। इनमें से क्रोध, भय तथा कामवासना की प्रवृत्तियाँ और संवेग अत्यधिक प्रबल हैं, जिनके दमन से या केन्द्रीकरण से असन्तुलन पैदा होता है। वस्तुतः मानसिक स्वस्थ्य की समस्या मूल-प्रवृत्ति संवेग (Instinct emotion) की समस्या है। जब व्यक्ति में कोई प्रवृत्ति जाग्रत होती है। तो उससे सम्बन्धित संवेग भी जाग जाता है
उदाहरणार्थ :
आत्म-स्थापन के साथ गर्व का, पलायन के साथ भय का तथा कामवृत्ति के साथ वासना का संवेग जाग्रत होता है। जाग्रत संवेग की असन्तुष्टि ही मानसिक रोग को जन्म देती है।
4. पारिवारिक कारण :
कुछ घरों में माता या पिता अथवा दोनों के अभाव से अथवा विमाता या विपिता के होने से बच्चे को पूरा पालन-पोषण, सुरक्षापूर्ण बरताव या स्नेह नहीं मिलता। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं और वे अभावग्रस्त बने रहते हैं। कहीं-कहीं माता-पिता के लड़ाई-झगड़े के कारण कलह का वातावरणं रहता है, जिसकी वजह से बालक को मानसिक घुटन अनुभव होती है और वह घर से दूर भागता है। इस प्रकार ‘भग्न परिवार (Broken House) मानसिक अस्वस्थता का मुख्य कारण बनता है।
5. विद्यालयी कारण :
बालकों का मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने का एक प्रमुख कारण विद्यालय भी हैं। जिन विद्यालयों में बच्चों पर कठोरतम अनुशासन थोपा जाता है, बच्चों को अकारण डाँट-फटकार या कठोर दण्ड सहने पड़ते हैं, अध्यापकों का स्नेह नहीं मिल पाता, पाठ्य विषय अनुपयुक्त होते हैं तथा बालकों को अमनोवैज्ञानिक विधियों से पढ़ाया जाता है, अध्यापक यो प्रबन्धक बच्चों को अपनी स्वार्थसिद्धि में भड़काकर आपस में या अध्यापकों से लड़ा देते हैं। ऐसे विद्यालयों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है।
6. सामाजिक कारण :
कभी-कभी कुछ समाज-विरोधी तत्त्व व्यक्ति के मन पर भारी आघात पहुँचाकर उसे मानसिक दृष्टि से असन्तुलित कर देते हैं। यदि व्यक्ति के कार्यों व विचारों का व्यर्थ ही विरोध किया जाए तो उसके मित्रों, पड़ोसियों तथा अन्य लोगों द्वारा उसे समाज में उचित मान्यता, स्थान या प्रतिष्ठान प्राप्त हो, तो उसमें प्रायः हीनता की ग्रन्थियाँ पड़ जाती हैं। उसका व्यक्तित्व कुण्ठा और तनाव का शिकार हो जाता है। आत्म-स्थापन की प्रवृत्ति के सन्तुष्ट न होने की वजह से भी व्यक्ति दुःखीं और खिन्न हो जाते हैं।
7. जीवन की विषम परिस्थितियाँ :
हूर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी-न-कभी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ निराशा और असफलताओं के कारण जन्म ले सकती हैं। आर्थिक संकट, व्यवसाय या परीक्षा या प्रेम में असफलता तथा सामजिक स्थिति के प्रति असन्तोष—इनसे सम्बन्धित प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियाँ मानव मन पर बुरा असर छोड़ती हैं। विषम परिस्थितियों के कारण समायोजन के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मानसिक अस्वस्थता सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं।
8. आर्थिक कारण :
“आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति की आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ अतृप्त रह जाती हैं और उसे अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। दमित इच्छाएँ नाना प्रकार के अपराध तथा समाज-विरोधी व्यवहार को जन्म देती हैं। धन की कमी से बाध्य होकर व्यक्ति को अधिक एवं अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उसका मन दु:खी रहता है। दुःखी मन मानसिक विकारों को पैदा करते हैं। अत्यधिक धन के कारण भी जुआ, शराब तथा वेश्यागमन की लत पड़ जाती है, जिससे मानसिक असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।
9. भौगोलिक कारण :
भौगोलिक कारण अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अधिक गर्मी या सर्दी के कारण लोगों का समायोजन बिगड़ जाता है, शारीरिक दशा गिरने लगती है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या तनाव पैदा होता है, जिससे मानसिक असन्तुलन उत्पन्न होता है।
10. सांस्कृतिक कारण :
यदा-कदा सांस्कृतिक परम्पराएँ व्यक्ति की भावनाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग में बाधक बनती हैं। प्रायः व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों का दमन कर कुछ कार्य विवशतावश करने पड़ते हैं, जिससे मानसिक असन्तोष तथा कुण्ठा उत्पन्न होती है। एक संस्कृति में जन्मा तथा पलता। हुआ व्यक्ति जब किसी दूसरी संस्कृति में कदम रखता है तो उसे मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिससे असमायोजन के दोष उत्पन्न होते हैं। अतः सांस्कृतिक कारणों से भी मनोविकार उत्पन्न होते हैं।
प्रश्न 4
मानसिके अस्वस्थता की रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम
यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः बलिक के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाये रखने के सभी सम्भव उपाय किये जाने चाहिए। मानसिक अस्वस्थता से बचाव तथा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने की दृष्टि से परिवार और पाठशाला की विशेष भूमिका है। इनका उल्लेख बारी-बारी से निम्न प्रकार किया गया है
(अ) परिवार और मानसिक स्वास्थ्य
परिवार के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत अंकित किया गया।
1. प्रारम्भिक विकास और सुरक्षा :
मानव जीवन के प्रारम्भिक 5-6 वर्षों में बालक का सर्वाधिक विकास हो जाता है। यह बालक की कलिकावस्था है, जिसे उचित सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। परिवार का इसमें विशेष दायित्व है, उसे शिशु की देख-रेख तथा रोगों से रक्षा करनी चाहिए। शिशु को सन्तुलित आहार दिया जाना चाहिए तथा उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। कुपोषण और असुरक्षा की भावना से बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
2. माता-पिता का स्नेह :
बालक के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उसे माता-पिता का प्रेम, स्नेह तथा लगाव मिलना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों को माता-पिता का भरपूर स्नेह नहीं मिलता, वे स्वयं को अकेला महसूस करते हैं तथा असुरक्षा की भावना से भय खाकर मानसिक ग्रन्थियों के शिकार हो जाते हैं। ये ग्रन्थियाँ स्थायी हो जाती हैं और उसे जीवन-पर्यन्त असन्तुलित रखती हैं।
3. परिवार के सदस्यों का व्यवहार :
परिवार के सदस्यों, खासतौर से माता-पिता का व्यवहार, सभी बालकों के साथ एकसमान होना चाहिए। उनके बीच पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना अनुचित है। उनकी असफलताओं के लिए भी बार-बार दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ता है और वे कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं।
4. उत्तम वातावरण :
परिवार का उत्तम एवं मधुर वातावरण बालक के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्यार, सहयोग की भावना, सम्मान की भावना व प्रतिष्ठा, एकमत्य, माता-पिता के मधुर सम्बन्ध तथा परिवार को स्वतन्त्र वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में योग देते हैं। इसके अलावा बालक की भावनाओं व विचारों को उचित आदर, मान्यता व स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।
5. संवेगात्मक विकास :
बालक को संवेगात्मक विकास भी ठीक ढंग से होना चाहिए। परिवार में यथोचित सुरक्षा, स्वतन्त्रता, स्वीकृति, मान्यता तथा स्नेह रहने से संवेगात्मक विकास स्वस्थ रूप से होता है तथा नये विश्वासों और आशाओं का जन्म होता है। बालक के स्वस्थ सांवेगिक विकास के लिए परिवार में पाँच मुख्य बातों का होना आवश्यक बताया गया है—आनन्द, खिलौने, खेल, पशु-पक्षी और उदाहरण (Joy, Tby, Play, Pet and Example) अधिक नियन्त्रण से भी संवेग विकसित नहीं हो पाते।
6. खेलकूदं और घूमना :
मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ गहरा सम्बन्ध है। परिवार को चाहिए कि बालकों के लिए खेलकूद का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाए। उन्हें दर्शनीय स्थल दिखाने, पिकनिक सर ले जाने, ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाने तथा भाँति-भाँति की वस्तुओं का निरीक्षण कराने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।
7. अनुशासन और अनुकरण :
बालक अधिकांश बातें अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण आदर्श वस्तु या विचार का होता है। अत: माता-पिता का जीवन अनुशासित एवं आदर्श जीवन होना चाहिए। परिवार से आत्मानुशासन की शिक्षा प्रदान की जाए।
(ब) पाठशाला और मानसिक स्वास्थ्य
बालक की दिनचर्या का अधिक समय परिवार में ही व्यतीत होता है। परिवार के बाद पाठशाला या विद्यालय की बारी है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने, मानसिक अस्वस्थता रोकने तथा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पाठशाला महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है
1. पाठशाला का वातावरण :
पाठशाला को सम्पूर्ण वातावरण शान्ति, सहयोग और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, विद्यार्थी के मन में अध्यापक के प्रति रुचि और आदर उत्पन्न करता है। इससे बालक स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक का भेदभावपूर्ण बरताव बालकों के मन में अनादर और खीझ को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक के निर्देशों की अवहेलना हो जाती है और परस्पर कुसमायोजन पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, पाठशाला में किसी प्रकार की राजनीति, गुटबाजी व साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इनसे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
2. श्रेष्ठ अनुशासन :
पाठशाला में अनुशासन को उद्देश्य बालकों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना है न कि उनके मन और जीवन को पीड़ा देना। अनुशासन सम्बन्धी नियम कठोर ने हों, उनसे बालकों में विरोध की भावना उत्पन्न न हो तथा उनका पालन सुगमता से कराया जा सके। बालकों को आत्मानुशासन के महत्त्व से परिचित कराया जाए, उन्हें अनुशासन समिति में स्थान देकर कार्य सौंपे जाएँ ताकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। इससे बालक का व्यक्तित्व विकसित व समायोजित होता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में योगदान मिलता है।
3. सन्तुलित पाठ्यक्रम :
बालकों के ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि तथा उनके बौद्धिक उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम का सन्तुलित होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम लचीला और बच्चों की रुचि के अनुरूप होजा चाहिए। रुचिजन्य अध्ययन से विद्यार्थियों को मानसिक थकान नहीं होती और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके विपरीत असन्तुलित पाठ्यक्रम के बोझ से बालक मानसिक थकान महसूस करते हैं, अध्ययन में कम रुचि लेते हैं तथा पढ़ने-लिखने से जी चुराते हैं। अतः सन्तुलित पाठ्यक्रम मानसिक सन्तुलन एवं स्वास्थ्य में सहायक है।
4. पाठ्य सहगामी क्रियाएँ :
पाठशाला में समय-समय पर पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। इनसे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उसकी रुचियों का उचित अभिप्रकाशन होता है। खेलकूद और मनोरंजन द्वारा मस्तिष्क में दमित भावनाओं को मार्ग मिलता है तथा मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
5. उपयुक्त शिक्षण विधियाँ :
पाठशाला में अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। नीरस शिक्षण से बालकों में अरुचि तथा थकान पैदा होती है, जिससे उनमें कक्षा से पलायन की प्रवृत्ति उभरती है तथा अनुशासनहीनता के अंकुर विकसित होते हैं।
6. शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन :
विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनकी मानसिक योग्यता तथा रुचि के अनुसार ही विषय दिये जाने चाहिए। इसके लिए कुशल मनोवैज्ञानिक द्वारा शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा उनके भावी जीवन को ध्यान में रखकर उन्हें उचित व्यवसाय चुनने हेतु भी परामर्श व दिशा-निर्देशन दिये जाएँ। व्यक्तिगत निर्देशन की सहायता से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, जिससे मानसिक ग्रन्थियाँ समाप्त हो जाती हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस प्रकार परिवार और पाठशाला अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वाह करके बालक की मानसिक उलझनों व तनावों को समाप्त या कम कर सकते हैं। इससे मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम सम्भव है। तथा मानसिक स्वास्थ्य का उचित संवर्धन सम्भव होता है।
प्रश्न 5
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के महत्त्व एवं उपयोगिता का भी उल्लेख कीजिए।
या
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अर्थ और महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसके विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। [2008]
या
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए। [2010]
या
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। [2007, 13, 15]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ व परिभाषा
सामान्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान या चिकित्साशास्त्र की बात की। जाती है, परन्तु आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को भी समान रूप से आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को जन्म देने का श्रेय सी० डब्ल्यू० बीयर्स (C. W. Bears) को प्राप्त है। सन् 1908 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मानसिक रोगों से ग्रस्त बस्तियों की दशा सुधारने के विषय में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था।
इसी वर्ष ‘मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान समिति (Association of Mental Hygiene) की स्थापना हुई। कुछ समय बाद इसी सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय परिषद् स्थापित की गयी। धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप में मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार हो गया। सन् 1930 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाशिंगटन (अमेरिका) में हुआ। कालान्तर में विश्व के सभी प्रगतिशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रचार व प्रसार होने लगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, मन के रोगों का निदान करने वाला विज्ञान, अर्थात् वह विज्ञान जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायता देता है।
शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बन्ध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से है, तो मानसिक वास्थ्य विज्ञान को सम्बन्ध मस्तिष्क से। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने तथा मानसिक रोगों का निदान और नियन्त्रण करने के उपाय बताता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसे मानसिक रोगों से मुक्त रखता है तथा यदि व्यक्ति मानसिक रोग या समायोजन के दोषों से ग्रस्त हो जाता है, तो उसके कारणों का निदान करके समुचित उपचार की व्यवस्था का प्रयास करता है।”
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं
- ड्रेवर के अनुसार, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है–मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसन्धान करना और उनकी सुरक्षा के उपाय करना।”
- क्रो एवं क्रो के अनुसार, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है, जो मानव कल्याण से सम्बन्धित है और मानव सम्बन्धों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है।”
- रोजानक के अनुसार, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति की मानसिक कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देता है तथा कठिनाइयों के समाधान के लिए साधन प्रस्तुत करता है।”
- हैडफील्ड के अनुसार, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है-मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक रोगों की रोकथाम।”
- भाटिया के अनुसार, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक रोगों से बचने और मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने का विज्ञान तथा कला है। यह कुसमायोजनाओं के सुधारों से सम्बन्धित है। इस कार्य में यह आवश्यक खेप से कारणों के निर्धारण का कार्य भी करता है।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्त्व या उपयोगिता या कार्य
मानसिक स्वास्थ्य एक लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। यह विज्ञानं मानसिक रोगियों की समस्याओं का समाधान तथा उनका उपचार करने की दिशा में एक वैज्ञानिक प्रयास है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण सहानुभूति, सहृदयतापूर्ण और सुधारवादी है। पेरिस (फ्रांस) के प्रसिद्ध कारागार चिकित्सक फिलिप पिने (Phillipe Pinel) ने सर्वप्रथम इन रोगियों को सुधारने के लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा नैतिक उपचार का मार्ग सुझाया। उसने मानसिक रोगियों की जंजीरें खुलवा दीं और उन्हें घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप बहुत-से रोगी अधिक सहयोगी व आज्ञाकारी बन गये और दूसरों के बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका समस्त श्रेय मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की विचारधारा को ही जाता है। वर्तमान समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का। महत्त्व निम्नलिखित है।
1. सन्तुलित व्यक्तित्व का विकास :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों-सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक आदि–को सन्तुलित रूप से विकसित होने के स्वस्थ सामाजिक जीवन का अवसर प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की मदद से मानसिक संघर्ष कम होता है तथा भावना ग्रन्थियाँ नहीं पनपने पातीं।
2. सुसमायोजित जीवन :
मनुष्य का सन्तुलित व्यक्तित्व उसे सन्तुलित जीवन जीने में मदद देता है। इससे व्यक्ति को सम-विषम परिस्थितियों को अनुकूलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। सन्तुलित जीवन के अवसर मिलने का अर्थ है–सुखी और सुसमायोजित जीवन-यापन का सौभाग्य प्राप्त होना।
3. स्वस्थ सामाजिक जीवन :
व्यक्ति समाज की इकाई है। सामागको एक और व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। समाज के सभी व्यक्तियों का सन्तुलित व्यक्तित्व तथा समायोजित जीवन सामाजिक जन को सौम्य एवं स्वस्थ बनाता है। ऐसे सन्तुलित समाज में सामाजिक विषमता और संघर्ष नहीं होंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक जीवन को स्वस्थ और सुन्दर बनाता है।
4. स्वस्थ पारिवारिक वातावरण :
स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण से पारिवारिक सन्तुलन सुसमायोजन, शान्ति-व्यवस्था और सुख में वृद्धि होती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से हर प्रकार के आनन्द तथा स्वस्थ वातावरण का सृजन होता है।
5. शिशुओं का समुचित पालन :
पोषण-मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के माध्यम से शिशुओं के माता-पिता एवं परिवारजन भली प्रकार यह समझ सकते हैं कि नवजात शिशुओं की देखभाल किस प्रकार की जाए। इससे शिशुओं की उचित सेवा-सुश्रूषा हो सकेगी तथा उनका विकास भी सुचारु रूप से हो सकेगा। यह पारिवारिक सन्तुलन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
6. शैक्षिक प्रगति :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियम और सिद्धान्त बालकों के स्वस्थ संवेगात्मक विकास में सहायक होते हैं। भावना ग्रन्थियों तथा मानसिक संघर्ष से मुक्त रहकर वे पास-पड़ोस तथा विद्यालय में समायोजन स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा के मार्ग में बाधक मानसिक रोग ग्रन्थियाँ हटने से शैक्षिक प्रगति सम्भव होती है।
7. उपचारात्मक महत्त्व :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मात्र स्वस्थ रहने और समायोजित जीवन व्यतीत करने सम्बन्धी नियम और सिद्धान्त ही निर्धारित नहीं करता, अपितु उपचार लेकर मानव-समाज की सेवा में उपस्थित होता है। रोकथाम और बचाव के साधन प्रयोग में लाने पर भी यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उसके प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था करता है।
8. व्यावसायिक सफलता :
व्यावसायिक सफलता के लिए व्यक्ति का जीवन सन्तुलित एवं समायोजित होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सन्तुलित व्यक्तित्व का सृजन करके व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करता है।
9. राष्ट्रीयता की भावना एवं सांवेगिक एकता :
विषमता और विघटनकारी प्रवृत्तियों के प्रभाव से वर्तमान परिस्थितियों में हमारा राष्ट्र सम्प्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि दूषित विचारधाराओं से जूझ रहा है। इससे राष्ट्रीय एकता भंग होती है तथा देश की शक्ति कमजोर पड़ती जाती है। इससे बचाव के लिए देश के नागरिकों में संवेगात्मक एकता का संचार करना होगा। यह कार्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की सक्रियता के अभाव में नहीं हो सकता।
10. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग :
अन्तर्राष्ट्रीय (या विश्व शान्ति के लिए आवश्यक है कि दुनिया के सभी देशों के नेतागण, चिन्तक, विचारक, समाज-सुधारक तथा नागरिक सन्तुलित और समायोजित व्यक्तित्व वाले हों। यदि देश के कर्णधारों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो विभिन्न देशों के बीच तनाव और संघर्ष निश्चित रूप से होगा। प्रायः एक ही व्यक्ति का असन्तुलित मस्तिष्क समूची मानव-संस्कृति को युद्ध एवं विनाश की अग्नि में झोंक देगा। उस असन्तुलिते मस्तिष्क के उपचार का दायित्व मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पर है। इससे विश्व-स्तर पर उत्पन्न तनाव और संघर्ष समाप्त होगा और विरोधी विचारधारा वाले देश निकट आकर मित्रता में बँध जाएँगे।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? इसका महत्त्व लिखिए। [2007, 08, 11, 12, 14]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य से आशय ‘मानव को अपने व्यवहार में सन्तुलन से है। यह सन्तुलन प्रत्येक अवस्था में बना रहना चाहिए। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की एक दशा एवं लक्षण है। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए उसके मन का स्वस्थ होना अतिआवश्यक है, क्योंकि मन द्वारा ही शरीर की समस्त क्रियाओं को संचालन किया जाता है। मन ही हमारे शरीर की बाह्य एवं आन्तरिक क्रियाओं को संचालित एवं नियन्त्रित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार, कार्यस्थल तथा अपने आस-पास के वातावरण से समायोजन स्थापित कर सुखी रहता है।
मानसिक स्वास्थ्य का महत्त्व
सामान्य रूप से माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, परन्तु यह मान्यता केवल आंशिक रूप से सत्य है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सम्पूर्ण स्वास्थ्य का प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष महत्त्व है। हम उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अधिक हद तक मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है तथा उससे प्रभावित होता है।
यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो, तो वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाता। इसके अतिरिक्त जीवन में प्रगति करने तथा समुचित आनन्द प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही भौतिक, दैहिक तथा आत्मिक रूप से सन्तुष्ट हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना। आवश्यक है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अति आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य तथा सीखने में सफलता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है।
वास्तव में सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए शिक्षार्थी तथा शिक्षक दोनों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को दृष्टिकोण सामान्य तथा सकारात्मक होता है। वह सभी कार्यों को पूर्ण उत्साह एवं लगन से सीखने को तत्पर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में नि:सन्देह सीखने की प्रक्रिया तीव्र तथा सुचारू होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी त्रुटियों के प्रति जागरूक होता है तथा उन्हें सुधारने का भी प्रयास करता है। इससे उसकी सीखने की प्रक्रिया अच्छे ढंग से चलती है। इन समस्त तथ्यों को ही ध्यान में रखते हुए क्रेन्डसन ने कहा है, “मानसिक स्वास्थ्य । और सीखने में सफलता का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है।”
उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी समान रूप से जागरूक रहना चाहिए तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हर सम्भव उपाय एवं प्रयास करना चाहिए। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की मौलिक मान्यताओं एवं नियमों तथा निर्देशों का पालन करके अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रख सकता है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि नियमित जीवन, समुचित व्यायाम तथा योगाभ्यास एवं जीवन के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रख सकता है तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है।
प्रश्न 2
मानसिक अस्वस्थता के क्या कारण हैं?
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने में विभिन्न कारकों का योगदान हो सकता है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।
1. मानसिक दुर्बलता :
ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, उनमें पर्याप्त ज्ञानात्मक योग्यता का अभाव पाया जाता है, ये व्यक्ति अक्सर मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं।
2. संवेगात्मक असन्तुलन :
संवेगात्मक असन्तुलन की स्थिति में व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है। यदि यह अवस्था निरन्तर बनी रहती है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है।
3. मानसिक संघर्ष :
स्थायी मानसिक संघर्ष अनेक बारे भयंकर रूप धारण कर लेते हैं तथा इनके कारण व्यक्ति असामान्य तथा गम्भीर मानसिक रोगी बन जाता है।
4. अत्यधिक थकान एवं काम का बोझ :
काम के अधिक बोझ एवं परिश्रम से व्यक्ति थक जाता है। निरन्तर बनी रहने वाली थकान मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करती है।
5. हीन भावना :
व्यक्ति में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हीन भावनाएँ जब एक ग्रन्थि का रूप धारण कर लेती हैं, तो ये ग्रन्थियाँ अनेक मानसिक विकारों को उत्पन्न करती हैं।
6. यौन-हताशाएँ :
यौन इच्छा की तृप्ति न हो पाने पर व्यक्ति प्राय: हताश हो जाते हैं। यह हताशा व्यक्ति को असामान्य बना देती है तथा व्यक्ति मानसिक रोगी, बन जाता है।
7. भावनाओं का दमन :
भावनाओं का दमन भी मानसिक अस्वस्थता का एक प्रमुख कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर विभिन्न प्रकार की भावनाएँ होती हैं, अनेक बार हर प्रकार की भावना को प्रदर्शित कर पाना सम्भव नहीं होता। दमित भावनाएँ अन्दर-ही-अन्दर सक्रिय रहती हैं, तथा भयंकर मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती हैं।
प्रश्न 3
मानसिक अस्वस्थता के निदान के उपायों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता के निदान के अन्तर्गत मानसिक अस्वस्थता के कारणों का पता लगाने के लिए रोगी के व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का प्राप्त करना आवश्यक है। ये सूचनाएँ इन बिन्दुओं से सम्बन्धित होती हैं।
- शारीरिक दशा
- पारिवारिक दशा
- शैक्षणिक दशा
- सामाजिक दशा
- आर्थिक दशा
- व्यावसायिक दशा
- व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षण तथा
- मानसिक तत्त्व।
इन सूचनाओं को निम्नलिखित विधियों की सहायता से उपलब्ध कराया जाता है
- प्रश्नावली
- साक्षात्कार
- निरीक्षण
- जीवनवृत्त
- व्यक्तित्व परिसूची
- डॉक्टरी जाँच
- विभिन्न मनोवैज्ञानिक (बुद्धि, रुचि, अभिरुचि तथा मानसिक योग्यता सम्बन्धी) परीक्षण
- विद्यालय का संचित आलेख
- प्रक्षेपण विधियाँ तथा
- प्रयोगात्मक एवं अन्वेषणात्मक विधियाँ।
प्रश्न 4
साधारण मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली सामान्य विधियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
सार्धारण मानसिक अस्वस्थता के उपचार में आवश्यकतानुसार निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है
1. सुझाव :
मानसिक रोगी को सीधे-सीधे सुझाव देकर समझाया जाए कि उसे अपनी अस्वस्थता के विषय में क्या सोचना व करना है। उसके भ्रम व भ्रान्तियों का भी निवारण किया जाए।
2. उन्नयन :
इस विधि में यह जाँच की जाती है कि मानसिक रोग का किस प्रवृत्ति या संवेग से सम्बन्ध है। फिर उसी प्रवृत्ति/संवेग का स्तर उन्नत करके उसे किसी उच्च लक्ष्य के साथ जोड़ दिया जाता
3. निद्रा :
अचानक आघात या दुर्घटना के कारण यदि कोई व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठा है तो रोगी को ओषधि देकर कई दिनों तक निद्रा में रखा जाता है। शरीर की ताकत को बनाये रखने की दृष्टि से ताकत के इंजेक्शन दिये जाते हैं।
4. विश्राम :
अधिक कार्यभार, थकावट, तनाव तथा मानसिक उलझनों और कुपोषण के कारणं अक्सर मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। ऐसे रोगियों को शान्त वातावरण में विश्राम करने हेतु रखा जाता है और उन्हें पौष्टिक भोजनं खिलाया जाता है।
5. पुनर्शिक्षण :
इसके अन्तर्गत मानसिक रोगी में व्यावहारिक शिक्षा, संसूचन तथा उपदेश के माध्यम से आत्मविश्वास व आत्म-नियन्त्रण पैदा किया जाता है। इसके लिए अन्य व्यक्ति, समूह या दैवी-शक्तियों में विश्वास के लिए भी उसे प्रेरित किया जा सकता है। इस विधि की सफलता रोगी द्वारा दिये गये सहयोग पर निर्भर करती है। कमजोर तथा कोमल भावनाओं वाले व्यक्तियों की इस विधि से चिकित्सा की जा सकती है।
6. ग्रन्थ विधि :
पढ़े-लिखे विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों के लिए ऐसे विशिष्ट ग्रन्थों की रचना की गयी है जिनके पढ़ने से मानसिक तनावे व असन्तुलन घटता है। रोग के अनुसार सम्बन्धित ग्रन्थ पढ़ने के लिए दिया जाता है और इसके पश्चात् उचित निर्देशन प्रदान कर रोग का पूर्व उपचार कर दिया जाता है।
प्रश्न 5
गम्भीर मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
गम्भीर मानसिक अस्वस्थता का उपचार साधारण विधियों के माध्यम से सम्भव नहीं है। इसके लिए रोगी को दीर्घकाल तक मानसिक रोग चिकित्सालय में किसी अनुभवी चिकित्सक की देख-रेख में रहना पड़ सकता है। इसके लिए अग्रलिखित विधियाँ प्रयुक्त होती हैं
1. आघात विधि :
पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को सुंघाकर रोगी के मस्तिष्क को आघात (Shock) दिया जाता था, जिससे क्षणिक लाभ होता था। इसके बाद अधिक मात्रा में इन्सुलिन या कपूर या मेट्राजॉल के द्वारा आघात दिया जाने लगा। रोगी को 15 से 60 तक आघात पहुँचाये जाते हैं। आजकल रोगी के मस्तिष्क पर बिजली के हल्के आघात देकर मानसिक रोग ठीक किये जाते हैं।
2. रासायनिक विधि :
रासायनिक विधि (Chemo Therapy) में कुछ विशेष प्रकार की ओषधियों या रसायनों का प्रयोग करके रोगी की चिन्ता तथा बेचैनी कम की जाती है। भारत में आजकल सर्पगन्धा (Rauwolfia) नामक ओषधि काफी प्रचलित व लाभदायक सिद्ध हुई है।
3. मनोशल्य चिकित्सा :
मनोशल्य चिकित्सा (Psycho-Surgery) के अन्तर्गत मस्तिष्क का ऑपरेशन करके थैलेमस व फ्रण्टल लोब के सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया जाता है। इससे मानसिक उन्माद और विकृतियाँ ठीक हो जाती हैं। यह देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद दूसरी मानसिक असामान्यताएँ पैदा हो जाती हैं। यह विधि सुधारे की दृष्टि से उपयुक्त कही जा सकती है, किन्तु इससे पूर्ण उपचार नहीं हो सकता।
प्रश्न 6
“अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह अपने विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर सकता।” यदि आप इस कथन से सहमत हैं, तो क्यों ? मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर :
विद्यालय में अध्यापक की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा दायित्व होता है। घर में बच्चों के लिए जो स्थान माता-पिता का होता है, विद्यालय में वही स्थान शिक्षक या अध्यापक का होता है। अध्यापक का दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ-ही-साथ उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के उत्तम विकास में भी भरपूर योगदान प्रदान करे। इस स्थिति में यह अनिवार्य है कि अध्यापक अपने विषय में पारंगत होने के साथ-ही-साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो।
यदि अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव उसके विद्यार्थियों के विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं तथा प्रभावित होते हैं। ऐसे में मानसिक रूप से अस्वस्थ अध्यापक के सम्पर्क में आने वाले विद्यार्थी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि “अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वह अपने विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर सकता।”
प्रश्न 7.
अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। [2010]
उत्तर :
शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा छात्रों के सामान्य एवं उत्तम विकास के लिए अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य सामान्य होना अति आवश्यक है, परन्तु व्यवहार में देखा गया है कि अनेक अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। वास्तव में विभिन्न कारक अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव डालते रहते हैं। इस प्रकार के मुख्य कारक हैं
- वेतन का कम होना
- सेवाओं को सुरक्षित न होना
- समाज में समुचित प्रतिष्ठा न होना
- विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक उपकरणों को उपलब्ध न होना
- कार्य-भार को अधिक होना
- विद्यालय का वातावरण अच्छा न होना
- प्रधानाचार्य और प्रबन्धकों से विवाद
- स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध न होना
- पारिवारिक प्रतिकूल परिस्थितियाँ तथा
- आवासीय समस्याएँ।
प्रश्न 8
‘मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में अध्यापक (विद्यालय) की भूमिका की विवेचना कीजिए। [2011]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान’ वह विज्ञान है, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसे मानसिक रोगों से मुक्त रखता है तथा यदि व्यक्ति मानसिक विकार, रोग अथवा समायोजन के दोषों से ग्रस्त हो जाता है तो उसके कारणों का निदान करके समुचित उपचार की व्यवस्था का प्रयास करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। इस विज्ञान द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के कार्य किये जाते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं
- मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा
- मानसिक रोगों की रोकथाम तथा
- मानसिक रोगों का प्रारम्भिक उपचार।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा ड्रेवर ने इन शब्दों में प्रतिपादित की है, “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है-मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसको सुरक्षित रखने के उपाय करना।” बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार करने में विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी जाती है। सर्वप्रथम विद्यालय का वातावरण उत्तम, सौहार्दपूर्ण तथा हर प्रकार की राजनीति, गुटबाजी तथा साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यालय में श्रेष्ठ अनुशासन बनाये रखें।
उन्हें मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। बालकों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाये रखने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियों को ही अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बालकों के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बालकों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता रहेगा तथा वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
प्रश्न 9
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक स्वास्थ्य में क्या अन्तर है? [2012, 15]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक दशा है, जब कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उस मानसिक दिशा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन दोनों में अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है
- मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं सन्तुलित क्रियाशीलता को कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्तित्व की इस क्रियाशीलता का अध्ययन करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति को बताता है। यह स्थिति दो प्रकार की हो सकती है-
मानसिक स्वस्थता तथा मानसिक अस्वस्थता। इन स्थितियों का अध्ययन करने वाला विषय ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों, मानसिक अस्वस्थता के लक्षणों, मानसिक रोग तथा उनके कारणों और मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के उपायों का अध्ययन व विवेचन करता है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर ही शिक्षण प्रक्रिया की गतिशीलता निर्भर करती है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
मानसिक स्वास्थ्य के तीन पक्ष कौन-से हैं?
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य के तीन पक्ष निम्नलिखित हैं
- प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, क्षमताओं, शक्तियों तथा अर्जित क्षमताओं को प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए।
- व्यक्ति की क्षमताओं में पारस्परिक समायोजन होना चाहिए।
- व्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियाँ एवं कार्य किसी उद्देश्य की ओर सक्रिय होने चाहिए।
प्रश्न 2
मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है?
या
मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। [2007, 15]
उत्तर :
स्वास्थ्य का प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्त्व है। हम उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अधिक हद तक मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है तथा उससे प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो, तो वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाता। इसके अतिरिक्त जीवन में प्रगति करने तथा समुचित आनन्द प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना। आवश्यक है।
प्रश्न 3
मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता का क्या सम्बन्ध है?
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य तथा सीखने में सफलता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए शिक्षार्थी तथा शिक्षक दोनों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का दृष्टिकोण सामान्य तथा सकारात्मक होता है। वह सभी कार्यों को पूर्ण उत्साह एवं लगन से सीखने को तत्पर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में नि:संदेह सीखने की प्रक्रिया तीव्र तथा सुचारु होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी त्रुटियों के प्रति जागरूक होता है तथा उन्हें सुधारने का भी प्रयास करता है। इससे उसकी सीखने की प्रक्रिया अच्छे ढंग से चलती है। इन समस्त तथ्यों को ही ध्यान में रखते हुए क्रेन्डसन ने कहा है, “मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है।”
प्रश्न 4
मानसिक रोगों के उपचार की व्यावसायिक चिकित्सा का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
खाली मस्तिष्क शैतान का घर है, किन्तु कार्य में रत व्यक्ति में कई विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं; जैसे—सहयोग, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य और मैत्री। इन गुणों से मानसिक उलझन और तनाव में कमी आती है। इसी सिद्धान्त को आधार बनाकर रोगियों को उनके पसन्द के कार्यों (जैसे—चित्रकारी, चटाई-कपड़ा-निवाड़, बुनना, टोकरी बनाना आदि) में लगा दिया जाता है, जिससे धीरे-धीरे उनका मानसिक सन्तुलन सुधर जाता है।
प्रश्न 5
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली सामूहिक चिकित्सा का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली सामूहिक चिकित्सा विधि में दस से लेकर तीस तक समलिंगी रोगियों की एक साथ चिकित्सा की जाती है। चिकित्सक समूह के सभी रोगियों को इस प्रकार प्रेरित करता है कि वे एक-दूसरे से अपनी समस्याएँ कहें तथा दूसरों की समस्याएँ खुद सुनें। एक-दूसरे को समस्या कहने-सुनने से पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न होती है। रोगी जब अपने जैसे अन्य पीड़ित व्यक्तियों को अपने साथ पाता है तो उसे सन्तोष अनुभव होता है। धीरे-धीरे चिकित्सक के दिशा-निर्देशन में सभी रोगी मिलकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं और मानसिक सन्तुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं।
प्रश्न 6
मानसिक रोगियों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली खेल एवं संगीत विधि का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
बालकों तथा दीर्घकाल तक दबाव महसूस क़रने वाले मानसिक रोगी व्यक्तियों के लिए खेल विधि उपयोगी है-रोगी को स्वेच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक नाना प्रकार के खेल खेलने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। खेल खेलने से उसकी विचार की दिशा बदलती है तथा खेल जीतने से उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार संगीत भी मानसिक उलझनों तथा तनावों को दूर करने की एक महत्त्वपूर्ण कुंजी है। रुचि का संगीत सुनने से उत्तेजित स्नायुओं को आराम मिलता है, संवेगात्मक उत्तेजनाओं का अन्त होता है, पाचन क्रिया तथा रक्तचाप सामान्य हो जाते हैं।
प्रश्न 7
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली मनो-अभिनय नामक विधि का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली एक सफल एवं लोकप्रिय विधि है-मनो-अभिनय विधि। मनो-अभिनय विधि (Psychodrarma), सामूहिक विधि से मिलती-जुलती विधि है। इसमें समूह के रोगी आपस में समस्या की व्याख्या नहीं करते, बल्कि अभिनय के माध्यम से अपनी समस्या का स्वतन्त्र रूप से अभिप्रकाशन करते हैं। इससे समस्या का रेचन हो जाता है। मनो-अभिनय चिकित्सक के निर्देशन में किया जाना चाहिए।
प्रश्न 8
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली सम्मोहन विधि का सामान्य परिचय दीजिए।
उत्तर :
सम्मोहन, अल्पकालीन प्रभाव वाली एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जिससे मनोरोग के लक्षण दूर होते हैं, रोग दूर नहीं होता। सम्मोहन क्रिया में चिकित्सक मानसिक रोगी को कुछ समय के लिए अचेत कर देता है और उसे एक आरामकुर्सी पर विश्रामपूर्वक बिठलाता है। अब उसे किसी ध्वन्यात्मक या दृष्टात्मक उत्तेजना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा जाता है। संसूचनाओं के माध्यम से उसे अचेत ही रखा जाता है। रोगी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी स्मृति से लुप्त हो चुकी अनुभूतियों को कहे। अनुभूति के स्मरण मात्र से ही रोगी का रोग दूर हो जाती है।
प्रश्न 9
मानसिक रोगों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली मनोविश्लेषण विधि का सामान्य वर्णन कीजिए।
उत्तर :
फ्रायड (Freud) नामक विख्यात मनोवैज्ञानिक ने सम्मोहन विधि की कमियों को ध्यानावस्थित रखते हुए ‘मनोविश्लेषण विधि (Psychoanalysis) की खोज की। रोगी को एक अर्द्ध-प्रकाशित कक्ष में आरामकुर्सी पर इस प्रकार विश्रामपूर्वक बिठलाया जाता है कि मनोविश्लेषक तो रोगी की क्रियाओं को पूर्णरूपेण अध्ययन व निरीक्षण कर पाये, लेकिन रोगी उसे न देख सके। अब मनोविश्लेषक के व्यवहार से प्रेरित व सन्तुष्ट व्यक्ति उस पर पूरी तरह विश्वास प्रदर्शित करता है। यद्यपि शुरू में प्रतिरोध की अवस्था के कारण रोगी कुछ व्यक्त करना नहीं चाहता, किन्तु उत्तेजके शब्दों के प्रयोग से उसे पूर्व-अनुभव दोहराने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद स्थानान्तरण की अवस्था के अन्तर्गत दो बातें हैं-
- रोगी चिकित्सक को भला-बुरा या गाली बकता है अथवा
- रोगी मनोविश्लेषक पर मुग्ध हो जाता है और उसकी हर बात मानता है।
शनैः – शनै: रोगी अपनी समस्त जानकारी मनोविश्लेषक को दे देता है, जिससे उसकी उलझनें समाप्त हो जाती हैं और वह सामान्य व समायोजित हो जाता है।
प्रश्न 10
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? [2007, 13, 14, 15]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं
- क्रो एवं क्रो के अनुसार, मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियन्त्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है, जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियन्त्रित किया जा सके।
- प्रत्येक व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायता देना।
- मानसिक तनाव और चिन्ताओं से मुक्ति दिलाने में सहायता देना।
प्रश्न 11
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य पक्षों का उल्लेख कीजिए।
या
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सकारात्मक पक्ष क्या है?
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के तीन प्रमुख पक्ष हैं
1. सकारात्मक पक्ष :
सकारात्मक पक्ष में उन नियमों तथा परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है जिनके द्वारा मनुष्य व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करते हुए जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सके। इनमें मानसिक रोगों की खोज करना तथा उनकी रोकथाम करना आते हैं।
2. नकारात्मक पक्ष :
मानसिक रोगों की सहानुभूतिपूर्ण ढंग से तथा कुशलता से चिकित्सा करना, उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना जिनके कारण मानसिक संघर्ष तथा भावना-ग्रन्थियों के उत्पन्न होने की सम्भावना होती रहती है।
3. संरक्षणात्मक पक्ष :
व्यक्ति को उन विधियों का ज्ञान कराना, जिनसे मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्ध को कायम रखा जा सकता है।
निश्चित उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक उत्तम परिभाषा दीजिए।”
उत्तर :
“मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है – मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसंधान करना और उनकी सुरक्षा के उपाय करना।” [ ड्रेवर ]
प्रटन 2
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य कार्य क्या हैं ? [2011]
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों, मानसिक अस्वस्थता के लक्षणों, मानसिक रोग तथा उनके कारणों और मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के उपायों का अध्ययन व विवेचन करता है।
प्रश्न 3
मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। [2008, 14]
उत्तर :
“मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की माँगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है।” -भाटिया
प्रश्न 4
मानसिक स्वास्थ्य और सीखने के बीच कैसा सम्बन्ध है?
उत्तर :
मानसिक स्वास्थ्य और सीखने के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की दशा में सीखने की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती है तथा मानसिक स्वास्थ्य के असामान्य हो जाने की दशा में सीखने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चल पाना सम्भव नहीं होता।
5
किस प्रकार आदमी (व्यक्ति) अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रख सकता है?
उत्तर :
कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का भली-भाँति पालन करके अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रख सकता है।
प्रश्न 6
मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है ?
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता वह स्थिति है जिसमें जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यक्ति स्वयं को असमर्थ पाता है तथा संवेगात्मक असन्तुलन का शिकार हो जाता है।
प्रश्न 7
मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है ?
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है – जीवन में समायोजन का बिगड़ जाना।
इन 8
‘स्वप्न विश्लेषण विधि किस उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है ?
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए स्वप्न विश्लेषण विधि’ को अपनाया जाता है।
प्रश्न 9
मानसिक रोगियों के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली मनोविश्लेषण विधि को किसने प्रारम्भ किया था ?
उत्तर :
मनोविश्लेषण विधि को फ्रॉयड (Freud) नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रारम्भ किया था।
प्रश्न 10
गम्भीर मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए अपनायी जाने वाली मुख्य विधियाँ कौन-कौन-सी हैं ?
उत्तर :
गम्भीर मानसिक अस्वस्थता के उपचार हेतु अपनायी जाने वाली मुख्य विधियाँ हैं।
- आघात विधि
- रासायनिक विधि तथा
- मनोशल्य चिकित्सा।
प्रश्न 11
मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन-सा है? [2015]
उत्तर :
जीवन में सामंजस्य तथा सकारात्मक सोच, मानसिक सोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
प्रश्न 12
हैडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बन्ध किससे है? [2013]
उत्तर :
हैडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बन्ध मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा मानसिक रोगों की रोकथाम है।
प्रश्न 13
मनोग्रन्थियों का निर्माण क्यों होता है? (2013)
उत्तर :
निरन्तर असफलताओं, हताशाओं, कुण्ठाओं तथा भावनाओं की अस्त-व्यस्तता के कारण मनोग्रन्थियों का निर्माण हो जाता है।
प्रश्न 14
निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के चार पहलू हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान केवल मानसिक रोगियों के लिए उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है।
- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन में सुसमायोजित होता है।
- बालक के मानसिक स्वास्थ्य में परिवार का कोई योगदान नहीं होता।
- मानसिक अस्वस्थता का कोई उपचार सम्भव नहीं है।
उत्तर :
- असत्य
- असत्य
- सत्य
- असत्य
- असत्य
बहुविकल्पीय प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों में दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए
प्रश्न 1.
“मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है – वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता।” यह परिभाषा दी है
(क) शेफर ने
(ख) लैण्डेल ने
(ग) मर्फी ने
(घ) ड्रेवर ने
उत्तर :
(ख) लैण्डेल ने
प्रश्न 2
“साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करता है। ऐसा कहा गया है
(क) ड्रेवर द्वारा
(ख) हैडफील्ड द्वारा
(ग) लैडेल द्वारा
(घ) कुप्पू स्वामी द्वारा
उत्तर :
(ख) हैडफील्ड द्वारा
प्रश्न 3
“मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है, जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव सम्बन्धों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह परिभाषा दी है
(क) क्री एवं क्रो ने
(ख) थॉमसन ने
(ग) शेफर ने
(घ) हैडफील्ड ने
उत्तर :
(क) क्रो एवं क्रो ने।
प्रश्न 4
“मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बन्ध मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने और मानसिक असन्तुलन को रोकने से है।” ऐसा कहा गया है
(क) हैडफील्ड द्वारा
(ख) क्रो और क्रो द्वारा
(ग) कुल्हन द्वारा
(घ) शेफर द्वारा
उत्तर :
(क) हैडफील्ड द्वारा
प्रश्न 5
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित पहलू हैं, सिवाय (2009)
(क) संरक्षणात्मक पहलू
(ख) सांस्कृतिक पहलू
(ग) उपचारांत्मक पहलू
(घ) निरोधात्मक पहलू
उत्तर :
(ख) सांस्कृतिक पहलू
प्रश्न 6
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्नलिखित कार्य नहीं है
(क) मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना
(ख) संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
(ग) मानसिक रोगों की रोकथाम करना
(घ) मानसिक रोगों का उपचार करना
उत्तर :
(ख) संक्रामक रोगों की रोकथाम करना
प्रश्न 7
मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है [2008, 12, 13]
(क) चिन्ता
(ख) निद्रा
(ग) तनाव
(घ) भग्नाशा
उत्तर :
(ख) निद्रा
प्रश्न 8
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है
(क) जीवन के कुछ क्षेत्रों में
(ख) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
(ग) जीवन के असामान्य क्षेत्र में
(घ) जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं
उत्तर :
(ख) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
प्रश्न 9
व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
(क) उसके सौन्दर्य का
(ख) उत्तम पोषण का
(ग) शारीरिक विकलांगता को
(घ) उच्च शिक्षा का
उत्तर :
(ग) शारीरिक विकलांगता का
प्रश्न 10
निम्नलिखित में से कौन-सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है?
(क) स्व-मूल्यांकन की योग्यता
(ख) समायोजनशीलता
(ग) आत्मविश्वास
(घ) संवेगात्मक अस्थिरता
उत्तर :
(घ) संवेगात्मक अस्थिरता
प्रश्न 11
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है [2007, 09, 11, 18]
(क) सामाजिक विकास करना
(ख) सांस्कृतिक विकास करना
(ग) मानसिक रोगों का उपचार करना
(घ) भावात्मक विकास करना
उत्तर :
(ग) मानसिक रोगों का उपचार करना
प्रश्न 12
निम्नलिखित में से कौन-सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण हैं? [2008]
(क) स्व-मूल्यांकन की योग्यता
(ख) समायोजनशीलता
(ग) आत्मविश्वास
(घ) ये सभी
उत्तर :
(घ) ये सभी
प्रश्न 13
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है [2013]
(क) उपचारात्मक पहलू
(ख) निरोधात्मक पहलू
(ग) संरक्षणात्मक पहलू
(घ) ये सभी
उत्तर :
(घ) ये सभी
प्रश्न 14
निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नहीं है? [2010, 13]
(क) अधिकतम प्रभावोत्पादक और सन्तुष्टि
(ख) जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना
(ग) व्यक्तियों का आपसी सामंजस्य
(घ) तेज गति से आर्थिक समृद्धि
उत्तर :
(घ) तेज गति से आर्थिक समृद्धि
प्रश्न 15
‘ए माइन्ड दैट फाउण्ड इटसेल्फ’ पुस्तक का सम्बन्ध है [2014]
(क) गणित से
(ख) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से
(ग) दर्शनशास्त्र से
(घ) विज्ञान से
उत्तर :
(ख) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से
प्रश्न 16
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है। [2016]
(क) आत्मविश्वास की अधिकता
(ख) तनाव की अधिकता
(ग) क्रोध की अधिकता
(घ) हर्ष की अधिकता
उत्तर :
(क) आत्मविश्वास की अधिकता
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 22 Mental Health and Mental Hygiene (मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Pedagogy Chapter 22 Mental Health and Mental Hygiene (मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.







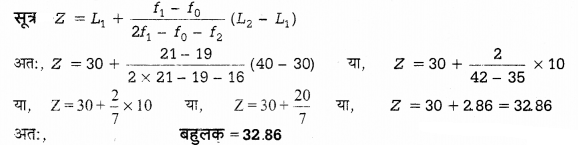
![]()
















![]()