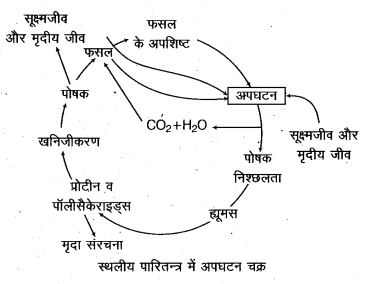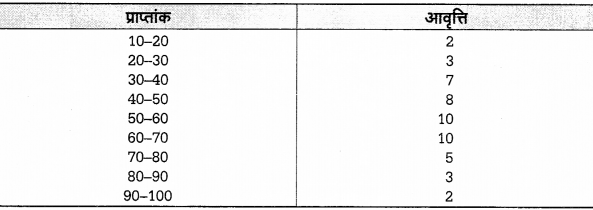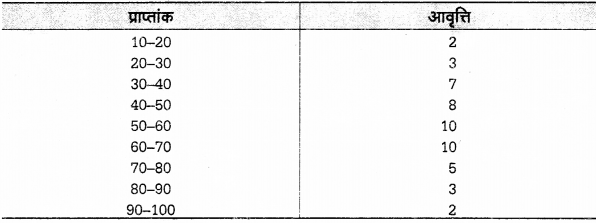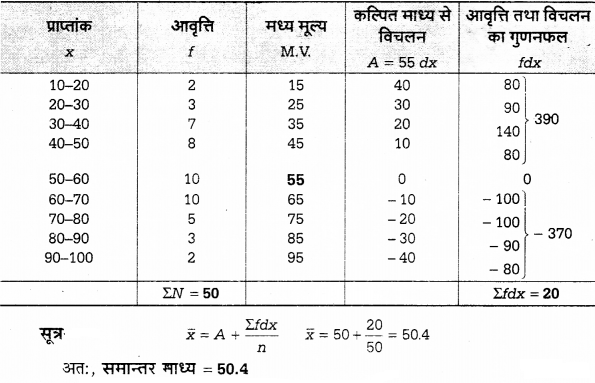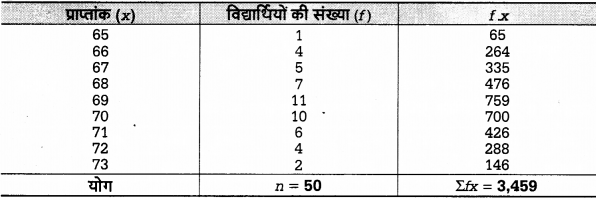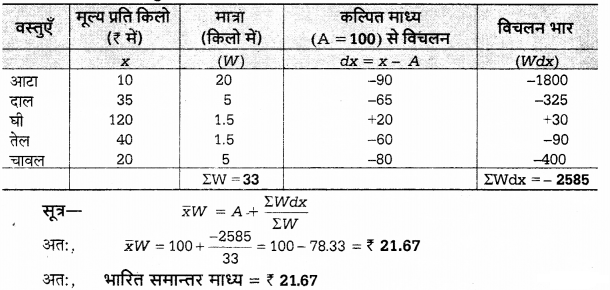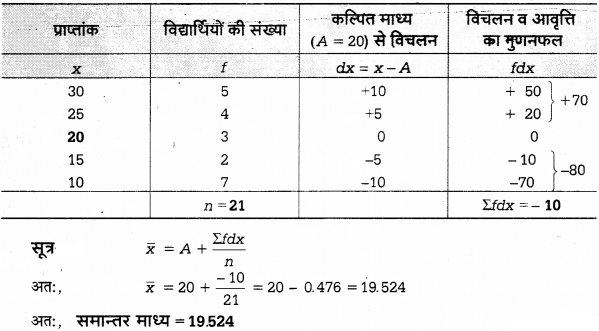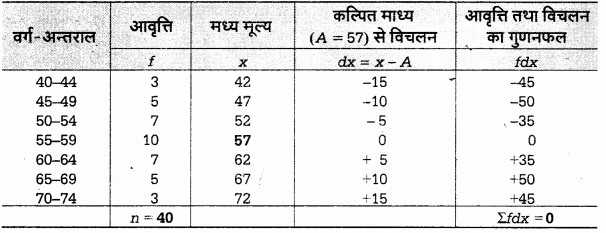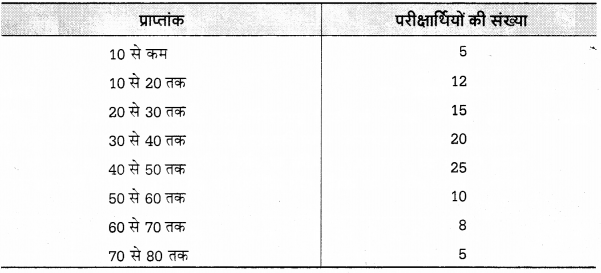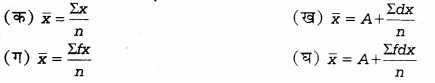UP Board Solutions for Class 12 Civics गुट-निरपेक्ष आन्दोलन are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics गुट-निरपेक्ष आन्दोलन.
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Civics |
| Chapter | 22 d |
| Chapter Name | गुट-निरपेक्ष आन्दोलन |
| Number of Questions Solved | 21 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Civics गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1
गुट-निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट-निरपेक्षता के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए।
या
गुट-निरपेक्षता के प्रमुख लक्षण बताइए। [2008, 10]
उत्तर :
गुट-निरपेक्षता
गुट-निरपेक्षता को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘तटस्थता’ के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार में तटस्थता का जो अर्थ लिया जाता है, गुट-निरपेक्षता उससे नितान्त भिन्न स्थिति है। तटस्थता और गुट-निरपेक्षता में भेद स्पष्ट करते हुए जॉर्ज लिस्का लिखते हैं –
“किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है किन्तु गुट-निरपेक्षता का आशय सही और गलत में विभेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना है।”
गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रणेता पं० नेहरू ने 1949 ई० में अमेरिकी जनता के सम्मुख कहा था –
जब स्वतन्त्रता के लिए संकट उत्पन्न हो, न्याय पर आघात पहुँचे या आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और न ही हम तटस्थ रहेंगे।” गुट-निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा, “हमारी तटस्थता का अर्थ है निष्पक्षता, जिसके अनुसार हम उन शक्तियों और कार्यों का समर्थन करते हैं जिन्हें हम उचित समझते हैं और उनकी निन्दा करते हैं जिन्हें हम अनुचित समझते हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा की पोषक हों।”
गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण
गुट-निरपेक्षता के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इस नीति के लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं –
1. शक्ति गुटों से पृथक रहने और महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौता न करने की नीति – गुट-निरपेक्षता का सबसे प्रमुख लक्षण है-शक्ति गुटों से पृथक् रहने की नीति। इसमें यह बात भी निहित है कि गुट-निरपेक्ष देश किसी भी महाशक्ति के साथ सैनिक समझौता नहीं करेगा। गुट-निरपेक्षता का मूल विचार है कि विश्व के देशों को परस्पर विरोधी शिविरों में विभक्त करने के प्रयासों या महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों के विस्तार के प्रयासों ने विश्व में तनाव की स्थिति को जन्म दिया है और गुट-निरपेक्षता का उद्देश्य इन शक्ति गुटों से अलग रहते हुए तनाव की शक्तियों को निर्बल करना है।
2. स्वतन्त्र विदेश नीति – गुट-निरपेक्षता का आशय यह है कि सम्बद्ध देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी शक्ति गुट के साथ बँधा हुआ नहीं है, वरन् उसका अपना स्वतन्त्र मार्ग है। जो सत्य, न्याय, औचित्य और शान्ति पर आधारित है। गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी का पिछलग्गू नहीं होता वरन् राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए सत्य, न्याय, औचित्य और विश्वशान्ति की प्रवृत्तियों का समर्थन करता है। स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन गुट-निरपेक्षता की नीति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इस नीति के कारण ही प्रत्येक गुट-निरपेक्ष देश प्रत्येक वैश्विक मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करता है।
3. शान्ति की नीति – गुट-निरपेक्षता का उदय विश्वशान्ति की आकांक्षा और उद्देश्य से हुआ है। यह शान्ति के उद्देश्यों और संकल्पों की अभिव्यक्ति है। इसका लक्ष्य है, तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शान्ति का विस्तार। गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भारत ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों (कोरिया, कांगो, साइप्रस) में शान्ति स्थापना के प्रयत्न किये और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा था, ‘गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इतिहास का सबसे बड़ा शान्ति आन्दोलन है।’
4. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति – गुट-निरपेक्षता साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, रंगभेद और शोषण तथा आधिपत्य के सभी रूपों का विरोध करने वाली नीति है। गुट-निरपेक्षता विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, समानता और विकास में विश्वास करती है; संघर्ष, अन्याय, दमन और असहिष्णुता का विरोध करती है एवं भूख तथा अभाव की स्थितियों को दूर करने पर बल देती है। विश्व के अनेक क्षेत्रों यथा एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
5. निरन्तर विकासशील नीति – गुट-निरपेक्षता एक स्थिर नीति नहीं वरन् निरन्तर विकासशील नीति है जिसे अपनाते हुए सम्बद्ध देशों द्वारा राष्ट्रीय हित और विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपने दृष्टिकोण और कार्य-शैली में परिवर्तन किया जा सकता है। 1971 की ‘भारत-सोवियत रूस मैत्री सन्धि’ गुट-निरपेक्षता की विकासशीलता की। परिचायक है। गुट-निरपेक्षता के समस्त सन्दर्भ में भी विकासशीलता का परिचय मिलता है। 1975 के पूर्व गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में राजनीतिक विषयों पर अधिक बल दिया जाता था। पिछले एक दशक में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्तर्गत आर्थिक विषयों और आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।
6. गुट-निरपेक्षता एक आन्दोलन है, गुट नहीं – गुट-निरपेक्षता एक गुट नहीं वरन् एक आन्दोलन है। एक ऐसा आन्दोलन, जो राष्ट्रों के बीच स्वैच्छिक सहयोग चाहता है, प्रतिद्वन्द्विता या टकराव नहीं।
7. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र का सहायक है, विकल्प नहीं – गुट-निरपेक्षता का विश्वास है कि “संयुक्त राष्ट्र के बिना आज के विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र का विकल्प या उसका प्रतिद्वन्द्वी नहीं वरन् इस संगठन की सहायक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली बनाना।”
![]()
प्रश्न 2.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को प्रारम्भ करने का क्या उद्देश्य था ? वर्तमान परिस्थितियों में इसका क्या महत्त्व है ? [2007, 12]
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा वर्तमान परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर एक निबन्ध लिखिए। [2014]
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कब और किसके द्वारा प्रारम्भ किया गया? वर्तमान विश्व की परिवर्तनशील परिस्थितियों में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए [2013]
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को पं० जवाहरलाल नेहरू के योगदान का उल्लेख कीजिए। [2014]
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
गुट-निरपेक्षता का आशय है, “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक गुट की सदस्यता या किसी भी महाशक्ति के साथ द्वि-पक्षीय सैनिक समझौते से दूर रहते हुए शान्ति, न्याय और राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त पर आधारित स्वतन्त्र रीति-नीति का अवलम्बन।”
गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ) – गुट-निरपेक्षता का सबसे प्रमुख लक्षण है-शक्ति गुटों से पृथक् रहने की नीति। गुट-निरपेक्ष देश का स्वतन्त्र मार्ग होता है तथा वह अन्तरष्ट्रिीय राजनीति में किसी का पिछलग्गू नहीं होता। गुट-निरपेक्षता का लक्ष्य है–तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शान्ति का विस्तार। गुट-निरपेक्षता साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, रंग-भेद और शोषण तथा आधिपत्य के सभी रूपों का विरोध करने वाली नीति है। गुट-निरपेक्षता एक गुट नहीं वरन् एक आन्दोलन है तथा निरन्तर विकासशील नीति है। गुट-निरपेक्षता को यह भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के बिना आज के विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती।
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को प्रारम्भ करने का उद्देश्य – वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्ष अथवा असंलग्नता का सिद्धान्त अत्यन्त प्रभावशाली और लोकप्रिय बन गया है। गुटनिरपेक्षता की नीति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय भारत को प्राप्त है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य विश्व का दो विरोधी गुटों में बँट जाना था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे गुट का नेता था सोवियत संघ। इन दोनों गुटों के बीच मतभेदों की एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गयी थी और दोनों गुट एक-दूसरे के विरोध में इस प्रकार सक्रिय थे कि इसे शीतयुद्ध का नाम दिया गया। 1947 ई० में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो एशिया और विश्व में भारत की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों विरोधी गुटों के देशों द्वारा भारत को अपनी ओर शामिल करने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये गये और परस्पर विरोधी गुटों के इन प्रयासों ने वैदेशिक नीति के क्षेत्र में भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भारत के द्वारा अपने विवेकपूर्ण मार्ग का शीघ्र ही चुनाव कर लिया गया और वह मार्ग था, गुट-निरपेक्षता अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए विश्व शान्ति, सत्य और न्याय का समर्थन करने की स्वतन्त्र, विदेश नीति।
प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता को सही रूप में नहीं समझा जा सका। केवल दो महाशक्तियों ने इसे ‘अवसरवादी नीति’ बतलाया, वरन् अन्य देशों द्वारा भी यह सोचा गया कि ‘आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरपेक्षता का कोई मार्ग नहीं हो सकता। लेकिन समय के साथ भ्रान्तियाँ कमजोर पड़ीं और शीघ्र ही कुछ देश गुट-निरपेक्षता की ओर आकर्षित हुए। ऐसे देशों में सबसे प्रमुख थे—मार्शल टीटो के नेतृत्व में यूगोस्लाविया और कर्नल नासिर के नेतृत्व में मिस्र। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता की एक त्रिमूर्ति बन गयी ‘नेहरू, नासिर और टीटो’। कालान्तर में, एशियाई-अफ्रीकी देशों ने सोचा कि गुट-निरपेक्षता को अपनाना न केवल सम्भव है, वरन् उनके लिए यह लगभग स्वाभाविक और उचित मार्ग है। 1961 ई० में 25 देशों ने इस मार्ग को अपनाया।
लेकिन अब इस आन्दोलन से जुड़े सदस्य देशों की संख्या 120 हो गयी है। ‘गुट-निरपेक्षता’। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे अधिक लोकप्रिय धारणा बन गयी है और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान ले लिया है।
वर्तमान में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व
बदलती परिस्थितियों में गुट-निरपेक्षता का स्वरूप भी बदला है, किन्तु इसका महत्त्व पहले से अधिक हो गया है। यही कारण है कि आज गुट-निरपेक्षता का पालन करने वाले राष्ट्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज प्रबल बन सकी है। विश्व के दो प्रतिस्पर्धी गुटों में सन्तुलन पैदा करने और विश्व-शान्ति बनाये रखने में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में ‘निर्गुट आन्दोलन (NAM) पर महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गयी है। आज की परिस्थितियों में निर्गुट देश ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने और बनाये रखने में योग दे सकते हैं।
विश्व के परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने और रंगभेद की नीति का विरोध करने में निर्गुट आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आज निर्गुट आन्दोलन निर्धन और पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। गुट-निरपेक्ष देशों की यह बराबर माँग रही है कि विश्व की ऐसी आर्थिक रचना हो, जिसमें विश्व की सम्पत्ति का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो सके। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की मान्यता है ‘आर्थिक शोषण का अन्त किये बिना’ विश्व-शान्ति सम्भव नहीं है। विश्व में शान्ति, स्वतन्त्रता और न्याय की रक्षा के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस आन्दोलन ने विश्व में तनाव, शैथिल्य में पर्याप्त योग दिया है। तीसरी दुनिया के आर्थिक विकास के लिए यह आन्दोलन आशा की किरण है। श्रीमती गाँधी ने निर्गुट आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन में ठीक ही कहा था-“गुट-निरपेक्षता का जो रूप था वह बदल गया है, किन्तु गुट-निरपेक्षता का युग नहीं बीता है।” उन्होंने आगे कहा-“गुट- निरपेक्षता मानव-व्यवहार का दर्शन है। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए बल-प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। गुट-निरपेक्षता का औचित्य कल भी उतना ही रहेगा, जितना आज है।”
[ संकेत – गुट-निरपेक्षता आन्दोलन में भारत की भूमिका हेतु लघु उत्तरीय प्रश्न (150 शब्द) प्रश्न 1 का अध्ययन करें। ]
प्रश्न 3.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [2010, 16]
या
क्या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आज भी प्रासंगिक है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। [2014, 16]
या
आधुनिक विश्व के सन्दर्भ में गुटनिरपेक्षता की सार्थकता पर एक निबन्ध लिखिए। [2012]
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उपादेयता (सार्थकता)
वर्तमान समय में बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत-से राजनीतिक विचारकों का यह दृष्टिकोण है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उपादेयता समाप्त हो चुकी है, अर्थात् गुटनिरपेक्ष आन्दोलन महत्त्वहीन हो गया है, अथवा आधुनिक परिस्थितियों में इस आन्दोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि आधुनिक परिस्थितियों में इस आन्दोलन को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
1. पहला दृष्टिकोण – गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अपनी उपादेयता खो चुका है-इस परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का कोई सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्त्व नहीं रह गया है। उनका यह मत इसे धारणा पर आधारित है कि 1991 ई० में सोवियत संघ के विघटन एवं शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना एवं विकास में शीतयुद्ध की राजनीति ने बहुत अधिक प्रभाव डाला था। एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों ने इस विचारधारा को इसलिए अपनाया था कि वे दोनों महाशक्तियों की गुटबन्दियों से पृथक् रहकर अपना विकास कर सकें एवं अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का संचालन कर सकें। परन्तु आधुनिक समय में विश्व राजनीति द्वि-ध्रुवीय के स्थान पर एक-ध्रुवीय अथवा बहु-ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो रही है। शक्ति के नये केन्द्र उदय हो रहे हैं। सैनिक शक्ति के स्थान पर आर्थिक शक्ति की महत्ता स्थापित होती जा रही है। क्षेत्रीय सहयोग के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था स्थिरता के स्थान पर गतिशील है। अतः ऐसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न-चिह्न लग गया है। शीतयुद्ध की राजनीति के कारण इस आन्दोलन का जन्म हुआ तथा जब शीतयुद्ध ही समाप्त हो गया है तो इस आन्दोलन का औचित्य निरर्थक है। अतः इसकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है।
2. दूसरा दृष्टिकोण : मजबूत बनने की दिशा में सक्रिय – कुछ विचारकों का यह मत है। कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उपादेयता है तथा इसको अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि स्वयं गुट-निरपेक्ष राष्ट्र अभी इन परिस्थितियों से हतोत्साहित नहीं हुए हैं, वरन् वे सक्रिय रूप से इसको सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व के राष्ट्र इसकी भूमिका के प्रति आशावान हैं; क्योंकि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या घटने के स्थान पर बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है सोलहवाँ शिखर सम्मेलन, जिसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 120 हो गयी है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर अमेरिका एवं पश्चिमी राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित है। ऐसे में इन विकासशील राष्ट्रों को संयुक्त संगठन की आवश्यकता है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इन राष्ट्रों की एकाधिकारवाद की भावना को चुनौती दे सके तथा अपने विकास सम्बन्धी नियमों एवं व्यवस्थाओं की स्थापना करवा सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्रों में 120 निर्गुट राष्ट्रों की स्थिति पर्याप्त महत्त्व रखती है और इन राष्ट्रों की सहमति के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। ये राष्ट्र कुछ सामान्य समस्याओं; जैसे-आतंकवाद, नशीली दवाओं के प्रयोग, जाति भेद, रंग-भेद, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, निरक्षरता आदि; से पीड़ित हैं। इनका समाधान इन राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है। यदि ये राष्ट्र संगठित होंगे तो ये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को काफी सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं।
3. भविष्य की सम्भावनाएँ – आधुनिक समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग २/३ सदस्य। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के हैं तथा इन्होंने इन अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से विश्व शान्ति, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के अन्त, रंगभेद की समाप्ति, परमाणु शस्त्रों पर रोक, नि:शस्त्रीकरण, हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करना आदि विषयों को उठाया, विचार-विमर्श किया तथा अनेक मुद्दों पर सफलताएँ भी प्राप्त की।
इस आन्दोलन के जन्म के पश्चात् से ही इसमें विसंगतियाँ आनी प्रारम्भ हो गयी थीं। इस आन्दोलन में धीरे-धीरे ऐसे राष्ट्रों का आगमन प्रारम्भ हो गया जो कि सोवियत संघ एवं अमेरिका से वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर जुड़ गए। क्यूबा साम्यवादी देश होने के बावजूद निर्गुट आन्दोलन से जुड़ गया। 1962 ई० में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो कोई भी गुट-निरपेक्ष राष्ट्र भारत की सहायता के लिए नहीं आया वरन् भारत को ब्रिटेन तथा अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त हुई। 1965 ई० में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत का पक्ष सोवियत संघ ने लिया। कश्मीर के मसले पर अनेक बार सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया। वियतनाम जैसे गुट-निरपेक्ष राष्ट्र पर 1979 ई० में चीन ने आक्रमण कर दिया और उसे सोवियत संघ से मैत्री करने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण तथा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का मूकदर्शक बना रहना इसकी सार्थकता को कम करता है। अत: इस आन्दोलन के विकास के साथ इसके अर्थ एवं परिभाषाएँ भी बदलनी प्रारम्भ हो गईं। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विदेश नीति की स्वतन्त्रता ही गुट-निरपेक्षता का एकमात्र मापदण्ड है। किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार की सन्धि करने पर गुट-निरपेक्षता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस आन्दोलन के जन्म के पश्चात् से ही इसमें विसंगतियाँ आनी प्रारम्भ हो गयी थीं। इस आन्दोलन में धीरे-धीरे ऐसे राष्ट्रों का आगमन प्रारम्भ हो गया जो कि सोवियत संघ एवं अमेरिका से वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर जुड़ गए। क्यूबा साम्यवादी देश होने के बावजूद निर्गुट आन्दोलन से जुड़ गया। 1962 ई० में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो कोई भी गुट-निरपेक्ष राष्ट्र भारत की सहायता के लिए नहीं आया वरन् भारत को ब्रिटेन तथा अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त हुई। 1965 ई० में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत का पक्ष सोवियत संघ ने लिया। कश्मीर के मसले पर अनेक बार सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया। वियतनाम जैसे गुट-निरपेक्ष राष्ट्र पर 1979 ई० में चीन ने आक्रमण कर दिया और उसे सोवियत संघ से मैत्री करने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण तथा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का मूकदर्शक बना रहना इसकी सार्थकता को कम करता है। अत: इस आन्दोलन के विकास के साथ इसके अर्थ एवं परिभाषाएँ भी बदलनी प्रारम्भ हो गईं। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विदेश नीति की स्वतन्त्रता ही गुट-निरपेक्षता का एकमात्र मापदण्ड है। किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार की सन्धि करने पर गुट-निरपेक्षता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की कमजोरी के लिए कुछ तो संरचनात्मक कमियाँ हैं; जैसे-स्थायी सचिवालय का न होना और इसके स्थान पर औपचारिक संगठनों; जैसे-समन्वय ब्यूरो तथा सम्मेलन; की स्थापना आदि उत्तरदायी हैं, तो दूसरी ओर सदस्य-राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेद, विवाद एवं संघर्ष इसकी संगठित शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य होने पर भी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अनेक सैनिक युद्ध हो चुके हैं और अभी भी अघोषित युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने की क्षमता तथा अमेरिका एवं चीन से अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने से भारत की शान्ति एवं सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यह सम्भव है कि भारत और पाकिस्तान का किसी भी समय भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो सकता है। भारत-चीन सीमा-विवाद, वियतनाम-कम्पूचिया विवाद, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ईरान-इराक विवाद, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण आदि अनेक समस्याएँ हैं जिनका कोई निश्चित समाधान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पास नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखायी देते हैं जहाँ इस आन्दोलन की आज भी प्रासंगिकता, उपादेयता एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका है; जैसे –
- नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास करना।
- उत्तर-दक्षिण संवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना।
- निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना।
- मादक द्रव्यों की तस्करी एवं आतंकवाद को रोकने में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास करना।
- दक्षिण-दक्षिण संवाद को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- एक-ध्रुवीय व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना।
![]()
प्रश्न 4.
गुट-निरपेक्षता की उपलब्धियों तथा विफलताओं का विवरण दीजिए। [2009, 10]
उत्तर :
गुट-निरपेक्षता की उपलब्धियाँ
गुट-निरपेक्षता विदेश-नीति का वह मूल सिद्धान्त है, जिसमें कोई भी राष्ट्र सम्मिलित हो सकता है। इस प्रकार गुट-निरपेक्षता का प्रादुर्भाव तथा विकास वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली नीति है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रमुख उपलब्धियों को अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है –
1. गुट-निरपेक्षता की नीति को मान्यता – विश्व के दोनों राष्ट्र-अमेरिका तथा सोवियत संघ यह समझते थे कि भुट-निरपेक्ष आन्दोलन सिवाय एक ‘धोखे’ के और कुछ नहीं है। अतः विश्व के राष्ट्रों को किसी एक गुट में अवश्य सम्मिलित हो जाना चाहिए, परन्तु गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अपनी नीतियों पर दृढ़ रहा। समय व्यतीत होने के साथ-साथ विश्व के दोनों गुटों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। साम्यवादी देशों का विश्वास साम्यवादी विचारधारा से हटकर एक नवीन स्वतन्त्र विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने विश्व में पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि गुट-निरपेक्ष देश वास्तव में स्वतन्त्र हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सोवियत संघ तथा गुट-निरपेक्ष देशों के समक्ष मूलभूत समस्याएँ समान हैं। पश्चिमी गुटों ने तो सातवें दशक में गुट-निरपेक्ष नीति को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों के प्रति सद्भावना तथा सम्मान का वातावरण उत्पन्न करने में आन्दोलनकारियों को जो सफलता प्राप्त हुई उसकी सराहना की जानी चाहिए।
2. शीत-युद्ध के भय को दूर करना – शीत-युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव का वातावरण व्याप्त था। परन्तु गुट-निरपेक्षता की नीति ने इस तनाव को शिथिलता की दशा में लाने के लिए भरसक प्रयत्न किया तथा इसमें सफलता भी प्राप्त की।
3. शीत-युद्ध को सक्रिय करना – अनेक गुट-निरपेक्ष देश चाहते थे कि विश्व के दोनों गुटों के मध्य शान्ति तथा सद्भावना का वातावरण बने। शीत-युद्ध के कारण अनेक देशों में भ्रम व्याप्त था कि यह शान्ति किसी भी समय युद्ध के रूप में भड़क सकती है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने शीत युद्ध को हथियारों के युद्ध में बदलने से रोका तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में व्याप्त भ्रम को दूर किया। सर्वोच्च शक्तियाँ समझ गईं कि व्यर्थ में रक्त बहाने से कोई लाभ नहीं है।
4. विश्व के संघर्षों को दूर करना – गुट-निरपेक्षता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने विश्व में होने वाले कुछ भयंकर संघर्षों को टाल दिया। धीरे-धीरे उनके निदान ढूंढ़ लिये गये। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने आणविक अस्त्र के खतरों को दूर करके अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान दिया। विश्व के छोटे-छोटे विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को दो भागों में विभाजित होने से रोका। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने सर्वोच्च शक्तियों को सदैव यही प्रेरणा दी कि “संघर्ष अपने हृदय में सर्वनाश लेकर चलता है इसलिए इससे बचकर चलने में विश्व का कल्याण है। इसके स्थान पर यदि सर्वोच्च शक्तियाँ विकासशील राष्ट्रों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करती हैं तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को बल मिलेगा।
5. अपनी प्रकृति के अनुसार पद्धतियों का आविष्कार करना – गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एक उपलब्धि यह भी है कि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे देशों की नीतियों को नकराते हुए अपनी प्रकृति के अनुकूल पद्धतियों का विकास किया। इस प्रकार भारत ने विश्व-बन्धुत्व, समाज-कल्याण तथा समाज के समाजवादी ढाँचे के अनुसार गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को चलने के लिए प्रेरित किया।
6. आर्थिक सहयोग का वातावरण बनाना – गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने विकासशील राष्ट्रों के बीच अपनी विश्वसनीयता का ठोस परिचय दिया जिसके कारण विकासशील राष्ट्रों को समय-समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकी। कोलम्बो शिखर सम्मेलन में तो आर्थिक घोषणा-पत्रे तैयार किया गया जिससे गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य अधिक-से-अधिक आर्थिक सहयोग की स्थिति निर्मित हो सके। एक प्रकार से गुट-निरपेक्षता का आन्दोलन आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है।
7. नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अपील – वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने नयी करवट बदली है। अत: नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की यह अपील तथा माँग है कि विश्व मंच पर ‘आर्थिक विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाए जो विश्व में व्यापार की स्थिति सुधारे, विकासशील राष्ट्रों को व्यापार करने के अवसर प्रदान करे, ‘सामान्य पहल’ के अनुसार गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी दोनों प्रकार का अनुदान प्राप्त हो। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की पहल के परिणामस्वरूप 1974 ई० में संयुक्त राष्ट्र संघ ने छठा विशेष अधिवेशन आयोजित किया जिसमें नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ समय बाद इस घोषणा-पत्र के विषय पर विकसित राष्ट्रों ने भी विचार-विमर्श किया, जो गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
8. निःशस्त्रीकरण तथा अस्त्र-नियन्त्रण की दिशा में भूमिका – गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों ने नि:शस्त्रीकरण तथा अस्त्र-नियन्त्रण के लिए विश्व में अवसर तैयार किया। यद्यपि इस क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों को तुरन्त सफलता नहीं मिली, तथापि विश्व के राष्ट्रों को यह विश्वास होने लगा कि हथियारों को बढ़ावा देने से विश्व-शान्ति संकट में पड़ सकती है। यह गुट-निरपेक्षता का ही परिणाम है कि 1954 ई० में आणविक अस्त्र के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा तथा 1963 ई० में आंशिक परीक्षण पर प्रतिबन्ध स्वीकार किए गए।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मान – गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदैव सम्मान किया, साथ ही संगठन के वास्तविक रूप को रूपान्तरित करने में भी सहयोग दिया। पहली बात तो यह है कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या इतनी है कि शीत-युद्ध के वातावरण को तटस्थता की नीति के रूप में परिवर्तन करने में राष्ट्रों के संगठन की बात सुनी गई। इससे छोटे राष्ट्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियन्त्रण सरलतापूर्वक लागू हो सका। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्त्व की वृद्धि करने में भी सहायता दी।
गुट-निरपेक्षता की विफलताएँ
गुट-निरपेक्षता की विफलताओं का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है –
1. सिद्धान्तहीन नीति – पश्चिमी आलोचकों का कहना है कि गुट-निरपेक्षता की नीति अवसरवादी तथा सिद्धान्तहीन है। ये देश साम्यवादी तथा पूँजीवादी देशों के साथ अवसरानुकूल ‘कार्य सम्पन्न करने में निपुण हैं। अत: ये देश दोहरी चाल चलते रहते हैं। इनका कोई निश्चित ध्येय नहीं है। ये देश अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों से नहीं चूकते हैं।
2. बाहरी आर्थिक तथा रक्षा सहायता पर निर्भरता – गुट-निरपेक्ष देशों पर विफलता का यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने बाहरी सहायता का आवरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। चूंकि वे हर प्रकार की सहायता चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मार्ग निकालकर अपना कार्य सिद्ध करने की नीति अपना ली है। आलोचकों का कहना है कि यदि गुट-निरपेक्षता की भावना सत्य पर आधारित होती तो ये देश आत्म-निर्भरता की नीति को मानकर चलते। अतः गुट-निरेपक्ष राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता के मार्ग में कील ठोंक दी है।
3. गुट-निरपेक्षता की नीति में सुरक्षा का अभाव – आलोचकों ने इस बात पर भी टीका टिप्पणी की है कि गुट-निरपेक्ष देश आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर संलग्न रहते हैं। ये देश सुरक्षा को पर्याप्त नहीं मानते हैं। ऐसी दशा में यदि वे बाहरी सैनिक सहायता स्वीकार करते हैं तो उनकी गुट-निरपेक्षता धरी की धरी रह जाएगी। सन् 1962 में चीन से आक्रमण के समय भारत को यह विदित हो गया कि बाहरी शक्ति के समक्ष गुट-निरपेक्ष राष्ट्र मुँह ताकते रह जाते हैं। इस प्रकार बाहरी शक्ति का सामना करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
4. अव्यावहारिक सिद्धान्तों की नीति – आलोचकों के कथनानुसार गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त अव्यावहारिक हैं। ये व्यवहार में विफल हुए हैं। सिद्धान्तों के अनुसार गुट-निरपेक्ष देशों को स्वतन्त्रता की नीतियों को सुदृढ़ करना था, परन्तु वे अपने दायित्व को निभाने में असफल रहे। पश्चिमी राष्ट्रों का तो यहाँ तक कहना है कि गुट-निरपेक्षता साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखती है परन्तु विश्व राजनीति में उसे गुप्त रखना चाहती है। पं० नेहरू ने सदा साम्यवादी रूस की प्रशंसा की तथा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण सोवियत संघ की नीतियों से प्रेरित होकर किया गया।
5. संकुचित नीति का पोषक – विदेश नीति का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। इस सम्बन्ध में आलोचकों का कहना है कि गुट-निरपेक्षता का सीमित वृत्त इतने व्यापक वृत्त को कैसे अपने में समेट सकता है। अतः गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एक प्रकार से अफसल है। गुटों से बाहर रहकर विश्व राजनीति में क्रियाशीलता का प्रदर्शन करना अत्यधिक कठिन है। विश्व की सम्पूर्ण नीति गुटों के चतुर्दिक घूमती है। अतः गुटों से पृथक् रहकर कोई भी राष्ट्र विकास के पथ पर नहीं पहुँच सकता।
6. राष्ट्रहित के स्थान पर नेतागिरी की नीति – कुछ आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता की भावना ऊर्ध्वगामी है, जबकि विश्व राजनीति की जड़ें अधोगामी हैं। ऐसी स्थिति में इस नीति के केन्द्र में राष्ट्रहित की भावना नहीं दिखाई देती है।
7. गुट-निरपेक्षता एक दिशाहीन आन्दोलन – कुछ आलोचकों का मानना है कि विश्व की नवीन मुक्त व्यापार की नीति के अन्तर्गत गुटे-निरपेक्षता का आन्दोलन निरर्थक सिद्ध हो रहा है। आज अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सद्भावना की आवश्यकता है, अलगावाद की नहीं। गुट-र्निरपेक्षता का आन्दोलन इस दृष्टि से दिशाहीनता का प्रदर्शन मात्र बनकर रह गया है।
8. गुट-निरपेक्षता की नीति से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं – आलोचकों का कहना है कि गुट-निरपेक्षता की नीति ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अभी तक कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया है। शीत-युद्ध के समय में सारा विश्व प्रमुख शिविरों में विभक्त रहा। इन शिविरों ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं के कहने में अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत के विरोध करने के पश्चात् भी अमेरिका ने कोरिया में अभियान चलाया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया तथा लेबनान में अमेरिकी सेनाएँ। प्रविष्ट हो गईं। पश्चिमी एशिया में अरब-इजराइल युद्ध हुए। इस प्रकार गुट-निरपेक्षता की नीति निरर्थक सिद्ध हुई।
इस प्रकार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का कोई ठोस आधार नहीं है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)
प्रश्न 1.
‘गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एवं भारत पर एक टिप्पणी लिखिए।
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका सदैव केन्द्रीय रही है। भारत के प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को इस आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है। 1947 से 1950 ई० तक पं० नेहरू के नेतृत्व में गुट-निरपेक्षता को सकारात्मक तटस्थता” के रूप में स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात् 1977 से 1979 ई० तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका व रूस दोनों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारों व= उनमें समन्वय स्थापित किया। इस काल को वास्तविक गुट-निरपेक्षता का काल कहा जाता है। 1980 ई० में भारत का नेतृत्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के हाथों में सौंपा गया। इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत ने 1983 ई० में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भाग लिया। इस काल में इन्दिरा गाँधी द्वारा दो समस्याओं पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें प्रथम, शीतयुद्ध को समाप्त करने तथा द्वितीय, परमाणु अस्त्रों की होड़ को समाप्त करने से सम्बन्धित थी। आठवाँ शिखर सम्मेलन जो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में सम्पन्न हुआ, में भारत का नेतृत्व प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी द्वारा किया गया था।
इस सम्मेलन में राजीव गाँधी द्वारा विकासशील राष्ट्रों के मध्य स्वतन्त्र संचार-प्रणाली’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त 1989 ई० में नवें शिखर सम्मेलन के समय भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी जिसके नेतृत्व में भारत द्वारा “पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में “पृथ्वी संरक्षण कोष’ की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1992 ई० में होने वाले दसवें शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा विश्व की प्रमुख समस्या परमाणु नि:शस्त्रीकरण वे राष्ट्रों के मध्य आर्थिक समानता कायम करने के प्रश्न को उठाया गया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जम्मू-कश्मीर जैसे भारत के द्विपक्षीय मसले पर बोलकर भारतीय भावनाओं के आन्दोलन की मूल भावनाओं को ठेस पहुँचायी। यद्यपि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नेल्सन मण्डेला के अध्यक्षीय भाषण की आलोचना की गयी व अपने कूटनीतिक चातुर्य के द्वारा उन्होंने सम्मेलन में भारत की साख को बचा लिया, परन्तु इस घटना ने भारत को भविष्य के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी।
प्रश्न 2.
गुटनिरपेक्षता का महत्त्व बताइए।
उत्तर :
गुटनिरपेक्षता का महत्त्व
वर्तमान विश्व के सन्दर्भ में गुटनिरपेक्षता का व्यापक महत्त्व है, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –
- गुटनिरपेक्षता ने तृतीय विश्वयुद्ध की सम्भावना को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अन्त करने और विश्व में शान्ति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- गुटनिरपेक्ष के कारण ही विश्व की महाशक्तियों के मध्य शक्ति-सन्तुलन बना रही।
- गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों ने सदस्य-राष्ट्रों के मध्य होने वाले युद्धों एवं विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान किया है।
- गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में एक-दूसरे को पर्याप्त सहयोग दिया है।
- गुटनिरपेक्षता ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व के परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र कराने और रंग-भेद की नीति का विरोध करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह आन्दोलन निर्धन तथा पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास पर बहुत बल दे रहा है।
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन राष्ट्रवाद को अन्तर्राष्ट्रवाद में परिवर्तित करने तथा द्विध्रुवीकरण को बहु-केन्द्रवाद में परिवर्तित करने का उपकरण बना।
- इसने सफलतापूर्वक यह दावा किया कि मानव जाति की आवश्यकता पूँजीवाद तथा साम्यवाद के मध्य विचारधारा सम्बन्धी विरोध से दूर है।
- इसने सार्वभौमिक व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शीत-युद्ध की भूमिका को कम करने तथा इसकी समाप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- गुटनिरपेक्षता नए राष्ट्रों के सम्बन्धों में स्वतन्त्रतापूर्वक विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करके तथा सदस्यता प्रदान करके उनकी सम्प्रभुता की सुरक्षा का साधन बनी है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)
प्रश्न 1.
‘गुट-निरपेक्षता की नीति के आवश्यक तत्त्व बताइए।
उत्तर :
गुट-निरपेक्षता की नीति के आवश्यक तत्त्व
सन् 1961 में बेलग्रेड में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में असंलग्नता की नीति के कर्णधारों-नेहरू, नासिर और टीटो ने इस नीति के 5 आवश्यक तत्त्व माने हैं, जो निम्नलिखित हैं
- सम्बद्ध देश स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करता हो।
- वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो।
- वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो।
- उसने किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता नहीं किया हो।
- उसने किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो।
उपर्युक्त आवश्यक तत्त्वों के अनुसार गुट-निरपेक्षता का आशय ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक गुट की सदस्यता या किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौते से दूर रहते हुए शान्ति, न्याय और राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त पर आधारित रीति-नीति का अवलम्बन है।
प्रश्न 2.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
- स्वतन्त्र राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक एकता व शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना हेतु।
- नवस्वतन्त्र राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक व तकनीकी सम्बन्धों की स्थापना करना।
- पर्यावरण प्रदूषण पर नियन्त्रण करना।
- स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
- साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद जैसी नीतियों का विरोध करना।
- मानव अधिकारों का समर्थन करना।
- निरस्त्रीकरण का समर्थन व युद्धों का विरोध करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने हेतु प्रयत्न करना।
- सैनिक गुटबन्दी से दूर रहना।
- परस्पर सहयोग द्वारा विकास की गति में वृद्धि करना।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
गुट-निरपेक्षता की त्रिमूर्ति से क्या आशय है?
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो संस्थापकों के नाम लिखिए। [2011, 13]
उत्तर :
गुट-निरपेक्षता की त्रिमूर्ति से आशय पं० जवाहरलाल (प्रधानमन्त्री भारत), कर्नल नासिर (राष्ट्रपति मिस्र) तथा मार्शल टीटो (राष्ट्रपति यूगोस्लाविया) से है।
प्रश्न 2.
गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ और कब सम्पन्न हुआ था? [2011]
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 ई० में हुआ था।
प्रश्न 3.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रणेता कौन थे? [2013]
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष की नीति के प्रणेता पं० जवाहरलाल नेहरू थे।
![]()
प्रश्न 4.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का 12वाँ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था?
उत्तर :
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का 12वाँ शिखर सम्मेलन डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में 1998 ई० में आयोजित हुआ था। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का 12वाँ विदेश मन्त्री सम्मेलन 1997 ई० में नयी दिल्ली में सम्पन्न हुआ था।
प्रश्न 5.
किन्हीं चार गुट-निरपेक्ष देशों के नाम अंकित कीजिए। [2007, 10, 11]
उत्तर :
भारत, मिस्र, मलेशिया एवं यूगोस्लाविया
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
गुट-निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किसने किया था ?
(क) इन्दिरा गाँधी ने
(ख) पं० जवाहरलाल नेहरू ने
(ग) लाल बहादुर शास्त्री ने
(घ) राजीव गाँधी ने
प्रश्न 2.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ? [2013]
(क) काठमाण्डू
(ख) कोलम्बो
(ग) बेलग्रेड
(घ) नयी दिल्ली
प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से कौन-सा एक गुट-निरपेक्ष देश नहीं है ? [2011, 14]
(क) ब्रिटेन
(ख) श्रीलंका
(ग) मिस्र
(घ) इण्डोनेशिया
प्रश्न 4.
गुट निरपेक्ष आन्दोलन नरम पड़ता जा रहा है क्योंकि [2012]
(क) इसके नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव है।
(ख) इसके सदस्य राष्ट्रों की सभी समस्याओं का समाधान हो गया है।
(ग) विश्व में अब एक ही गुट प्रभावशाली रह गया है।
(घ) गुट-निरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक हो गया है।
प्रश्न 5.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की नींव कब पड़ी? [2013]
या
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। [2016]
(क) 1960
(ख) 1961
(ग) 1962
(घ) 1965
प्रश्न 6.
वर्ष 2012 में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? [2013]
(क) इराक
(ख) ईरान
(ग) चीन
(घ) अमेरिका
प्रश्न 7.
निम्नलिखित में से कौन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं है? [2012]
(क) मिस्र के कर्नल नासिर
(ख) यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो
(ग) भारत के पं० जवाहरलाल नेहरू
(घ) चीन के चाऊ-एनलाई
प्रश्न 8.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक नेता कौन थे? [2015]
(क) पं० मोतीलाल नेहरू, सुहात, यासर अराफात
(ख) इंदिरा गांधी, फिडेल कास्त्रो, कैनिथ कौन्डा
(ग) नासिर, जवाहरलाल नेहरू, टीटो।
(घ) श्रीमावो भण्डारनाईके, अनवर सदात, जुलियस नायरेरे
उत्तर :
- (ख) पं० जवाहरलाल नेहरू ने
- (ग) बेलग्रेड
- (क) ब्रिटेन
- (घ) गुटनिरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक हो गया है
- (ख) 1961
- (ख) ईरान
- (घ) चीन के चाऊ-एनलाई
- (ग) नासिर, जवाहरलाल नेहरू, टीटो।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Civics गुट-निरपेक्ष आन्दोलन help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Civics गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.