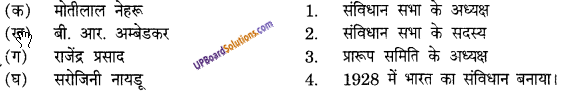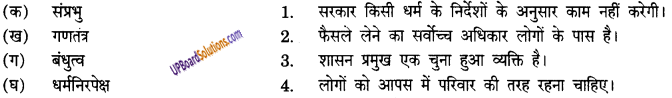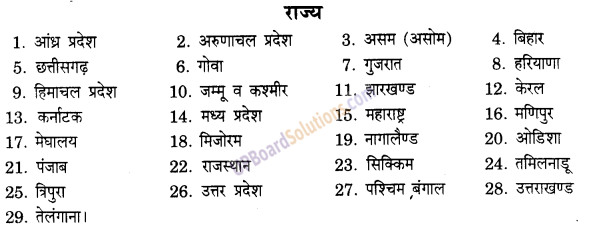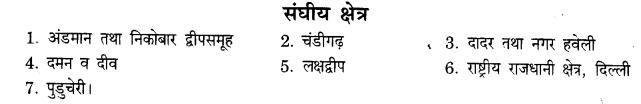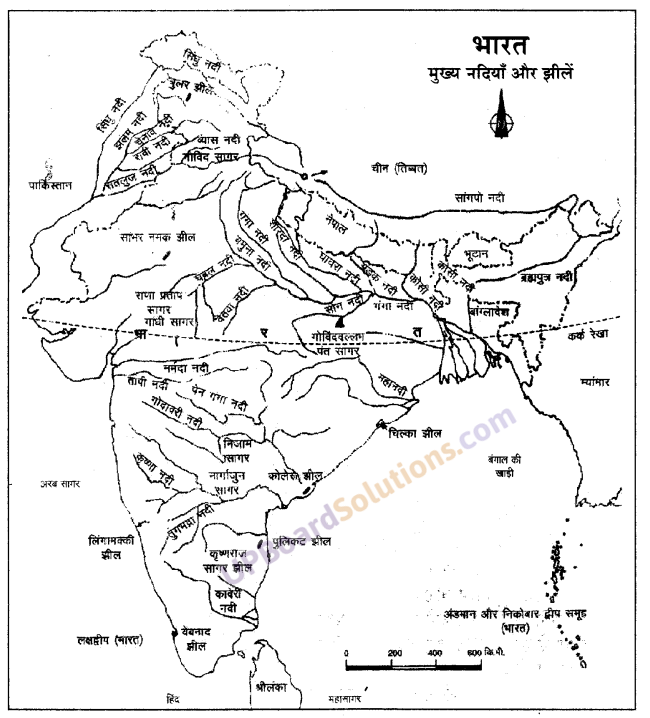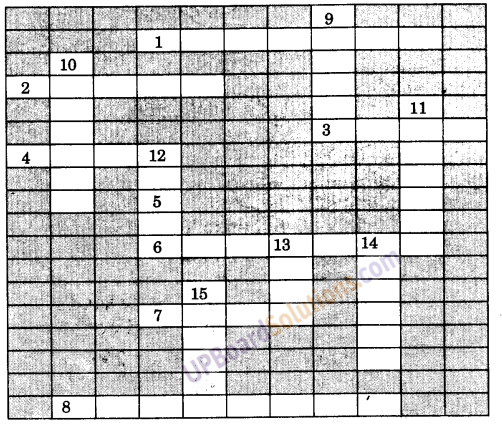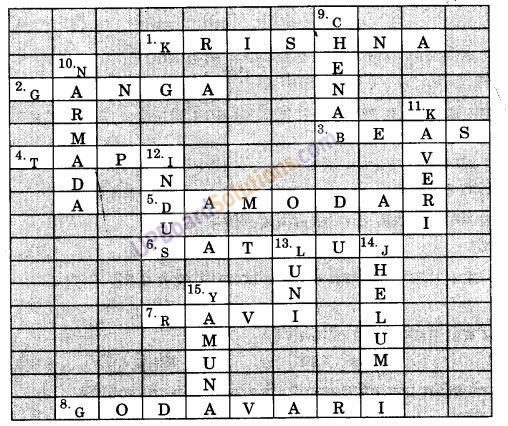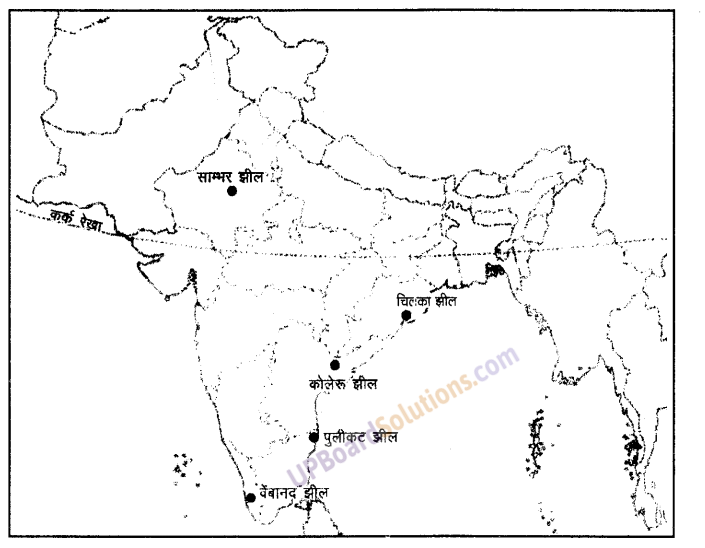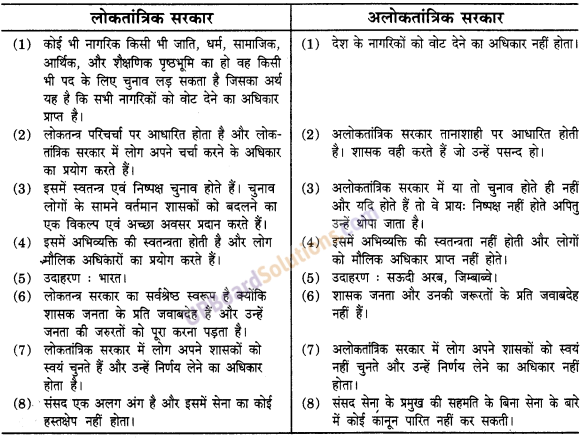UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रान्ति
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 9 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रान्ति.
पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 ई. से पहले कैसे थे?
अथवा
1905 ई. से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। इनमें कई देश गणराज्य थे, तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्ग ने ले लिया था। परन्तु रूस अभी भी ‘पुरानी दुनिया में जी (UPBoardSolutions.com) रहा था। यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी –
1. 1905 ई. से पूर्व रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति-
(i) किसानों की शोचनीय स्थिति- रूस में किसानों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। वहाँ कृषि-दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, लेकिन किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी कृषि जोतें बहुत ही छोटी थीं और खेती को विकसित तरीके से करने के लिए उनके पास पूँजी का अभाव था। इन छोटी-छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी।
(ii) श्रमिकों की हीन दशा- औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में बड़े-बड़े पूँजीपतियों ने अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरम्भ कर दिया। वे उन्हें कम वेतन देते थे तथा कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि बच्चों व स्त्रियों के जीवन से भी खिलवाड़ करने में वे कभी नहीं चूकते थे। ऐसी अवस्था से बचने के लिए मजदूर एक होने लगे। किन्तु 1900 ई. में इन पर (UPBoardSolutions.com) हड़ताल करने व संघ बनाने पर भी रोक लगा दी गई। उन्हें न तो कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही उन्हें सुधारों की कोई आशा थी। ऐसे समय में उनके पास मरने अथवा मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
यूरोप के देशों की तुलना में रूस में औद्योगीकरण बहुत देर से शुरू हुआ। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए थे। रूस में उद्योग-धन्धे लगाने के लिए पूँजी का अभाव होने के कारण विदेशी पूँजीपति रूस के धन को लूटकर स्वदेश पहुँचाते रहे। सन् 1904 मजदूरों के लिए बहुत बुरा था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए। मजदूरी 20 प्रतिशत घट गयी। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता था।
2. रूस की राजनीतिक स्थिति-रूस की राजनीतिक स्थिति 1905 ई. से पूर्व अत्यन्त चिंताजनक थी। रूस में जार का निरंकुश शासन था जिसमें जनता ‘पुरानी दुनिया की तरह रह रही थी क्योंकि वहाँ पर अभी तक यूरोप के अन्य देशों की भाँति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहे थे। रूस के किसान, श्रमिक और जनसाधारण की हालत बड़ी खराब थी। रूस में औद्योगीकरण देरी से हुआ। (UPBoardSolutions.com) सारा समाज विषमताओं से पीड़ित था। राज्य जनता को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं था क्योंकि वह दैवी सिद्धान्त में विश्वास रखता था। जार और उसकी पत्नी बुद्धिहीन और भोग-विलासी थे। वह जनता पर दमनपूर्ण शासन रखना चाहता था।
![]()
प्रश्न 2.
1917 ई. से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन-किन स्तरों पर भिन्न थी?
अथवा
1917 ई. से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी?
उत्तर:
रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से 1917 ई. से पहले भिन्न थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गाँव से शहर नहीं आए थे। इनमें से ज्यादातर गाँवों में ही रहना पसन्द करते थे और शहर में काम करने के निमित्त रोज गाँव से आते और शाम को वापस लौट जाते थे। वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बँटे हुए थे और यह उनकी (UPBoardSolutions.com) पोशाकों से परिलक्षित होता था। धातुकर्मी अपने को मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। क्योंकि उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी तथापि कामकाजी जनसंख्या कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल के मोर्चे पर एकजुट थी।
अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी।
कारखाना मजदूरों की स्थिति भी इतनी ही खराब थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे।
वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कार्य घण्टों की कोई सीमा नहीं थी जिसके (UPBoardSolutions.com) कारण उन्हें दिन में 12-15 घण्टे काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि न तो उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही सन् 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी।
किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। कुलीन वर्ग, सम्राट तथा रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। ब्रिटेन में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे किन्तु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला। तत्कालीन रूस के किसान अपनी कृषि भूमि एकत्र कर (UPBoardSolutions.com) अपने कम्यून (मीर) को सौंप देते थे और किसानों को कम्यून उस कृषि भूमि को प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार बाँट देता था, जिससे उस कृषि भूमि पर सुगमता से कृषि की जा सके।
प्रश्न 3.
1917 ई. में जार का शासन क्यों खत्म हो गया?
उत्तर:
जार की नीतियों के प्रति बढ़ते जन असन्तोष के कारण सन् 1917 में जार के शासन का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने रूस में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम परिवर्तित कर दिए तथा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे जन आक्रोश को निरस्त कर दिया। रूस में युद्ध तो अत्यधिक लोकप्रिय थे और जनता युद्ध में जार का साथ भी देती थी किन्तु जैसे-जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने (UPBoardSolutions.com) ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएँ प्रबल होने लगीं। जारीना अलेक्सान्द्रा के सलाहकारों विशेषकर रास्पूतिन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाई हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए जिससे हालात और बिगड़ गए।
प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बन्द हो गया। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 ई. तक रेलवे लाइनें टूट गईं। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमन्द लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम (UPBoardSolutions.com) बात हो गई। 26 फरवरी, 1917 ई. को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दाँव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च, 1917 ई. को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अन्त हो गया।
किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार को अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुण्ठा के कारण वे (UPBoardSolutions.com) आमतौर पर लगान देने से मना कर देते और प्रायः जमींदारों की हत्या करते। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी धारणा और सर्वहारा की विश्व-विजय के उद्घोष ने रूस के जारशाही से आक्रोशित लोगों को विद्रोह के लिए उद्वेलित किया।
![]()
प्रश्न 4.
दो सूचियाँ बनाइए : एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए।
उत्तर:
जार की गलत नीतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा जनसाधारण एवं सैनिकों की दुर्दशा के कारण रूस में क्रान्ति का वातावरण तैयार हो चुका था। एक छोटी-सी घटना ने इस क्रान्ति की शुरुआत कर दी और यह दो चरणों में पूरी हुई। ये दो चरण थे—फरवरी क्रान्ति और अक्टूबर क्रान्ति।
संक्षेप में क्रान्ति का सम्पूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है-
फरवरी क्रान्ति- 1917 ई. के फरवरी माह में शीतकाल में राजधानी पेत्रोग्राद में हालात बिगड़ गए। मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक कमी हो गयी जबकि संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। नगर की संरचना इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गयी। मजदूरों (UPBoardSolutions.com) के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएँ तट पर स्थित थे। बाएँ तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा वह महल भी था जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी।
सर्दी बहुत ज्यादा थी – असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। 22 फरवरी को दाएँ किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी हो गई। अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कई कारखानों में महिलाओं ने हड़ताल की अगुवाई की।
रविवार, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। गलियाँ रोटी, मजदूरी, बेहतर कार्य घण्टों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गईं।
घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रान्ति एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर पेत्रोग्राद सोवियत नाम की सोवियत या काउंसिल बना ली। । जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनैतिक दल नहीं था। इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया था। पेत्रोग्राद ने राजशाही का अन्त कर दिया और इस (UPBoardSolutions.com) प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।
फरवरी क्रान्ति का प्रभाव यह हुआ कि जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया। पेत्रोग्राद सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई यद्यपि इनमें एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। अप्रैल, 1917 ई. में बोल्शेविकों के नेता ब्लादिमीर लेनिन देश निकाले से रूस वापस लौट आए। उसने ‘अप्रैल थीसिस’ के नाम से जानी जाने वाली तीन माँगें रखीं। ये तीन माँगें थीं- युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रैडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए।
अक्टूबर क्रान्ति- जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण चार माँगें थीं- शांति, भूमि का स्वामित्व जोतने वालों को, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा गैर-रूसी जातियों को समानता का दर्जा। अस्थायी सरकार का प्रधान केरेस्की इनमें से किसी भी माँग को पूरा न कर सका और सरकार ने जनता का समर्थन खो दिया। लेनिन फरवरी क्रान्ति के समय स्विट्जरलैण्ड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, वह अप्रैल में रूस लौट आया। उसके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करने, किसानों को जमीन देने तथा ‘सारे अधिकार सोवियतों को देने (UPBoardSolutions.com) की स्पष्ट नीतियाँ सामने रखीं। गैर-रूसी जातियों के प्रश्न पर भी केवल लेनिन की बोल्शेविक पार्टी के पास एक स्पष्ट नीति थी। अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों में मतभेद के कारण हुई। सितम्बर में ब्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
16 अक्टूबर, 1917 ई. को उसने पेत्रोग्राद सोवियते तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉटस्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई।
जब 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ, प्रधानमंत्री केरेस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला; ऑरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया।
थोड़ी सी गम्भीर लड़ाई के उपरान्त बोल्शेविकों ने मॉस्को पेत्रोग्राद क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया। पेत्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की बैठक में बोल्शेविकों की कार्रवाई को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
अक्टूबर क्रान्ति का नेतृत्व मुख्यतः लेनिन तथा उसके (UPBoardSolutions.com) अधीनस्थ ट्रॉटस्की ने किया और इसमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे।
प्रश्न 5.
बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रान्ति के फौरन बाद कौन-कौन से प्रमुख परिवर्तन किए?
उत्तर:
अक्टूबर क्रांति के पश्चात् बोल्शेविकों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन- रूस की बागडोर अपने हाथ में लेकर बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध को समाप्त करने, किसानों को जमीन दिलाने तथा सम्पूर्ण सत्ता सोवियतों को सौंपने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीतियाँ अपनाईं। सबसे पहले रूस ने अपने-आपको प्रथम विश्वयुद्ध से बिलकुल अलग कर लिया चाहे इसके लिए उसे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। इसके पश्चात् जो-जो (UPBoardSolutions.com) उपनिवेश रूस के अधीन थे उन सब उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। तदुपरान्त बोल्शेविक पार्टी ने अनेक घोषणाएँ कीं जिनसे रूस में समाजवाद का सूत्रपात हुआ। यह घोषणाएँ निम्नलिखित थीं
- बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) रख दिया गया।
- नवम्बर में संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी, 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च, 1918 में राजनैतिक विरोध के बावजूद रूस ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली।
- रूस एक-दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया।।
- उन्होंने पहली बारे केन्द्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर, पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं।
- बोल्शेविक निजी सम्पत्ति के पक्षधर नहीं थे अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- भूमि को सामाजिक सम्पत्ति घोषित कर दिया गया (UPBoardSolutions.com) और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे।
- शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए।
- पुराने अभिजात्य वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई।
- परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियाँ पेश कीं।
![]()
प्रश्न 6.
निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए-
(क) कुलक
(ख) ड्यू मा
(ग) 1900 से 1930 ई. के बीच महिला कामगार
(घ) उदारवादी
(ङ) स्तालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम।
उत्तर:
(क) कुलक- ये सोवियत रूस के धनी किसान थे। कृषि के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्तालिन ने इनका अन्त कर दिया। स्तालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927-28 ई. तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत को सामना कर रहे थे। इसलिए इन कुलकों पर 1928 ई. में छापे मारे गए और उनके अनाज के भण्डारों को जब्त कर लिया गया। माक्र्सवादी स्तालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई और अन्ततः स्तालिन को इन कुलकों का सफाया। करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी।
(ख) ड्यूमा- ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में परिवर्तित कर दिया था। इसमें मात्र अनुदारवादी राजनीतिज्ञों को ही स्थान दिया गया। उदारवादियों तथा क्रान्तिकारियों को इससे दूर रखा गया।
(ग) 1900 से 1930 ई. के बीच महिला कामगार- महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन् 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31 प्रतिशत भाग बन चुकी थी किन्तु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम (UPBoardSolutions.com) मजदूरी दी जाती थी।
महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थीं। प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा भी देती थीं।
1917 ई. की अक्टूबर क्रान्ति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 ई. में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉरेंज टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासीलेवा ने बढ़ती कीमतों तथा कारखाने के मालिकों की मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी माफ वासीलेवा का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की तब तक उन्होंने राहत की साँस नहीं ली।।
(घ) उदारवादी- उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है, इसका सम्बन्ध न किसी एक युग से है और न ही किसी सर्वमान्य व्यक्ति विशेष से। यह तो युगों-युगों तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का परिणाम है। इस विचारधारा के समर्थक प्रायः निम्न विषयों में परिवर्तन चाहते थे
- उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले।
- व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए।
- नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे स्वेच्छाचारी शासन का अन्त हो सके तथा व्यक्ति का (UPBoardSolutions.com) विकास तीव्र गति से सम्भव हो सके।
- इनके अनुसार व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं का दास नहीं बनना चाहिए। प्रगति एवं विकास के लिए यदि परम्पराओं का विरोध करना पड़े तो भी करना चाहिए।
(ङ) स्तालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम- सन् 1929 से स्तालिन के साम्यवादी दल ने सभी किसानों को सामूहिक स्रोतों (कोलखोज) में काम करने का निर्देश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो-सामान को सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिल-जुलकर काम करते थे। कोलखोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बाँट दिया जाता था। इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध किया।
इस विरोध को जताने के लिए वे अपने जानवरों को मारने लगे। परिणामस्वरूप रूस में 1929 से 1931 ई. के बीच जानवरों की संख्या में एक तिहाई की कमी आयी। सरकार द्वारा सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था। अनेक विरोधियों को देश से निर्वासित कर दिया गया। (UPBoardSolutions.com) सामूहिकीकरण के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। दूसरी तरफ 1930 से 1933 ई. के बीच खराब फसल के बाद सोवियत रूस में सबसे बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में 40 लाख से अधिक लोग मारे गए।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था?
उत्तर:
कोलखोज।
![]()
प्रश्न 2.
रूस में बोल्शेविक दल का मुख्य नेता कौन था?
उत्तर:
रूस में बोल्शेविक दल का मुख्य नेता ब्लादिमीर इलिच उलियानोव (लेनिन) था।
प्रश्न 3.
1917 ई. में रूस पर किसका प्रभाव था?
उत्तर:
जार निकोलस द्वितीय का।
प्रश्न 4.
रूस में किस धर्म के अनुयायी बहुमत में थे?
उत्तर:
रूसी आर्थोडॉक्स क्रिश्चियैनिटी के।
प्रश्न 5.
कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो के लेखक का नाम बताइए।
उत्तर:
कार्ल मार्क्स एवं फ्रेड्रिक एंगेल्स।
प्रश्न 6.
कार्ल मार्क्स कौन था?
उत्तर:
यह आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। मूलतः जर्मन मार्क्स का ज्यादातर समय इंग्लैण्ड व यूरोपीय देशों में बीता। उसने अपने आजीवन साथी फ्रेड्रिक एंगेल्स से मिलकर प्रथम कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र तथा दास कैपिटल नामक विश्वविख्यात पुस्तक की रचना की।
प्रश्न 7.
रूसी क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
उत्तर:
उनका प्रमुख उद्देश्य था—
- रूस को प्रथम विश्व युद्ध से हटाना,
- कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण,
- गैर-रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना,
- जमीन जोतने वाले को देना।
प्रश्न 8.
रैडिकल से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
यूरोप में उन लोगों का समूह जो देश में ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो।
![]()
प्रश्न 9.
राष्ट्रवादी से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में यूरोप में उन्होंने उदारवादियों एवं रैडिकल का समर्थन किया। वे ऐसा देश चाहते थे जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले।
प्रश्न 10.
विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का नाम बताइए।
उत्तर:
ऑरोरा युद्धपोत।
प्रश्न 11.
रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया?
उत्तर:
25 फरवरी, 1917 ई. को।
प्रश्न 12.
किस घटना के बाद जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़ना पड़ा?
उत्तर:
घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। दूसरी रेजीमेंटों ने बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी।
प्रश्न 13.
घुमंतू तथा स्वायत्तता का अर्थ बताइए।
उत्तर:
घुमंतू-ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते रहते हैं। स्वायत्तता-अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार स्वायत्तता कहलाता है।
प्रश्न 14.
बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना में क्या प्रतिक्रिया हुई?
उत्तर:
जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे।
प्रश्न 15.
रूस की जनता का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न था?
उत्तर:
रूस की जनता का लगभग 85 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न था।
प्रश्न 16.
वास्तविक वेतन से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं।
![]()
प्रश्न 17.
खूनी रविवार से क्या समझते हैं?
उत्तर:
पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुँचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 18.
रैडिकल किस तरह की सरकार के पक्ष में थे?
उत्तर:
रैडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे।
प्रश्न 19.
1917 ई. से पहले रूस के दो प्रमुख औद्योगिक शहरों के नाम लिखिए।
उत्तर:
1917 ई. से पूर्व रूस के दो प्रमुख औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को थे।
प्रश्न 20.
रूढ़िवादी किस तरह के बदलाव चाहते थे?
उत्तर:
रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानि अठारहवीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन उन्नीसवीं सदी तक आते-आते वे भी मानने लगे थे। कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है परन्तु वह चाहते थे कि (UPBoardSolutions.com) अतीत का सम्मान किया जाय. अर्थात् अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो।
प्रश्न 21.
उदारवादी समूह किस तरह की सरकार के पक्षधर थे?
उत्तर:
उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के
अनुसार शासन कार्य चलाएँ।
![]()
प्रश्न 22.
रूस में स्थापित होने वाले प्रथम समाजवादी संगठन का नाम बताइए।
उत्तर:
‘रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्ल्स पार्टी (रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी) 1898 ई. में रूस में स्थापित होने वाला प्रथम समाजवादी संगठन था।
प्रश्न 23.
1904 ई. में सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूर हड़ताल पर क्यों चले गए थे?
उत्तर:
1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ एशियन वर्कर्स के चार सदस्यों को प्युतिलोव आयरन वक्र्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का एलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घण्टे घटाकर आठ घण्टे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की माँग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
प्रश्न 24.
रूसी क्रान्ति में सक्रिय दो प्रमुख दल कौन-से थे?
उत्तर:
- बोल्शेविक दल,
- मेन्शेविक दल।
प्रश्न 25.
रैडिकल और उदारवादियों की आर्थिक दशा किस प्रकार थी?
उत्तर:
बहुत सारे रैडिकल और उदारवादियों के पास काफी सम्पत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन-दौलत (UPBoardSolutions.com) इकट्ठा की थी इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए।
प्रश्न 26.
1905 ई. की क्रान्ति का आरम्भ किस घटना को माना जाता है?
उत्तर:
1905 ई. की क्रान्ति का आरम्भ ‘खूनी रविवार को माना जाता है।
प्रश्न 27.
किस कारण उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री-पुरुष उदारवादी और रैडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द-गिर्द गोलबंद हो गये थे?
उत्तर:
उदारवादियों और रैडिकल समूहों की मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूँजी है उन्हें बिना रोकटोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज (UPBoardSolutions.com) परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री-पुरुष उदारवादी और रैडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द-गिर्द गोलबंद हो गए थे।
![]()
प्रश्न 28.
अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी?
उत्तर:
अस्थायी रूसी सरकार प्रिंस केरेंस्की के नेतृत्व में बनी थी।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
समाजवाद की तीन विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
समाजवाद की तीन प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
- इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है।
- समाजवाद में समाज वर्गविहीन होता है। इसमें अमीर-गरीब के बीच कम-से-कम अन्तर होता है। इसी कारण समाजवाद निजी सम्पत्ति का विरोधी है।
- उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होता है।
प्रश्न 2.
केरेस्की की सरकार की अलोकप्रियता का कारण बताइए।
उत्तर:
रूस में जार के शासन का अन्त होने के बाद प्रिंस केरेस्की की सरकार अस्तित्व में आयी।
इसके सम्मुख प्रमुख समस्याएँ थीं-
- युद्ध की समस्या,
- भूमि की समस्या,
- औद्योगिक श्रमिकों की समस्या।
केरेंस्की की अलोकप्रियता के कारण- यद्यपि केरेंस्की एक योग्य नेता था, परन्तु वह इन समस्याओं को हल करने और जनता की माँगों को पूरा करने में असमर्थ रहा। इसीलिए मार्च, 1917 ई. की क्रांति के बाद रूस में जगह-जगह श्रमिक पंचायतों (सोवियतों) का निर्माण हो गया। इन पंचायतों ने केरेंस्की के स्थान पर स्वयं रूस का शासन संभालने का निश्चय किया। इसलिए वह अलोकप्रिय हो गया। 7 नवम्बर को (UPBoardSolutions.com) केरेंस्की सरकार का पतन हो गया और लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी जिसे ‘काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमीसार्स का नाम दिया गया।
प्रश्न 3.
रैडिकल और रूढ़िवादी में क्या अन्तर है? बताइए।
उत्तर:
(1) रूढ़िवादी- रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक राजतंत्र एवं राजा के दैवी सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। यह रैडिकल तथा उदारवादी दोनों विचारधाराओं का विरोध करते थे परन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त तक इनकी विचारधारा में तीव्र परिवर्तन आया और इन्होंने भी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया परन्तु यह चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो तथा अतीत को पूरी तरह न ठुकराया जाए।
(2) रैडिकल (आमूल परिवर्तनवादी )- इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों के यह विरोधी थे। यह राजा (UPBoardSolutions.com) के दैवी शक्ति के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे और राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के पक्ष में थे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारधारा के समर्थकों को जाता है।
प्रश्न 4.
बोल्शेविक और मेन्शेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अन्तर था?
उत्तर:
बोल्शेविक और मेन्शेविक के बीच निम्नलिखित अन्तर इस प्रकार है-
|
बोल्शेविक |
मेन्शेविक |
| 1. बोल्शेविक रूस में 1917 ई. में एक सफल क्रांति ला सके और उन्होंने देश तथा समाज का ढाँचा पूरी तरह करता था। | 1. किन्तु यह मेन्शेविक कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि रूसी जार संसदीय तरीकों में विश्वास नहीं बदल दिया। |
| 2. बोल्शेविक रूस में मजदूरों का बहुमत वाला समूह था जिसका नेता लेनिन था। वे समाज तथा देश में बदलाव के लिए संसदीय के लिए क्रान्तिकारी तरीकों में विश्वास करते थे। | 2. मेन्शेविक रूस में मजदूरों का एक दूसरा समूह था जो कि देश तथा समाज को चलाने तरीकों एवं चुनावों में भाग लेने में विश्वास रखता था। |
| 3. इन लोगों का मत था कि संसदीय तौर-तरीके रूस जैसे देश में बदलाव नहीं ला सकेंगे जहाँ लोकतंत्रात्मक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई संसद नहीं थी। | 3. ये लोग फ्रांस तथा जर्मनी में मौजूद दलों के पक्षधर थे जो कि अपने देशों में विधायिका के चुनावों में भाग लेते थे। |
प्रश्न 5.
साम्यवाद और फासिस्टवाद के बीच प्रमुख अन्तर बताइए।
उत्तर:
- साम्यवाद ने अन्तर्राष्ट्रीयता के विचार को उभारा है। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा में विश्वबन्धुत्व एवं अन्तर्राष्ट्रीयता प्रमुख है। जबकि फासिस्टवाद के अनुसार दो राष्ट्रों या कई राष्ट्रों के मध्य कोई समन्वय अथवा मेल नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने राष्ट्रीयता पर ही अधिक बल दिया।
- साम्यवाद ने जातिभेद, रंगभेद एवं लिंगभेद को यदि समाप्त नहीं, तो कम अवश्य कर दिया। साम्यवाद स्वतंत्रता, समानता एवं प्रजातंत्र पर आधारित है। दूसरी ओर फासिस्टवाद, समाजवाद एवं प्रजातंत्र का विरोधी है। यह संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करता। फासिज्म एवं प्रजातंत्र को परस्पर विरोधी माना जाता है। इसमें बहुमत के स्थान पर एक ही नेता की तानाशाही को अधिक महत्त्व दिया गया है।
![]()
प्रश्न 6.
खूनी रविवार और इसके बाद के घटनाक्रम को बताइए।
उत्तर:
जनवरी, 1905 ई. में रूसी शासक जार से याचना करने के लिए एक रविवार को मजदूरों ने पादरी गैपॉन के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। लेकिन ज्यों ही जुलूस विंटर पैलेस पहुँचा, पुलिस एवं कोसैक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक मजदूर मारे गए और कई घायल हो गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार ने घटनाओं की एक श्रृंखला को आरंभ कर दिया जिसे 1905 की क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में हड़तालों का आयोजन (UPBoardSolutions.com) किया गया। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए छात्रों ने बहिष्कार किया तो विश्वविद्यालय बन्द हो गए। वकीलों, इंजीनियरों, डॉक्टरों एवं अन्य मध्यम श्रेणी के मजदूरों ने यूनियन ऑफ यूनियन्स बनाया तथा एक संविधान सभा की माँग की।
प्रश्न 7.
रूसी क्रान्ति की सफलता के पश्चात् समाजवादी प्रणाली लोगों के लिए किस तरह उपयोगी थी? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
निस्संदेह रूसी क्रान्ति की सफलता के बाद रूस में समाजवादी प्रणाली की स्थापना हुई थी। यह प्रणाली कई कारणों की वजह से लोगों के लिए अच्छी थी जिनमें से चार प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर क्रांति के उपरांत स्थापित की गई समाजवादी प्रणाली लोकोपयोगी कही जा सकती है।
- नई प्रणाली में निजी सम्पत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबन्ध लगा दिया जोकि मूलतः पूँजीपतियों तथा मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के कारण पैदा होती है।
- रूसी क्रान्ति के बाद भूमि किसानों के पास तथा कारखाने मजदूरों के पास चले गए।
- समाजवादी प्रणाली ने लोगों को स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाकर उन्हें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के अधीन ला दिया।
- समाजवादी प्रणाली में हर व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया। शोषण बन्द हो गया तथा प्रत्येक नागरिक को काम प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिल गया। एक नए समाज का निर्माण हुआ जोकि सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित था।
प्रश्न 8.
रूस में उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे-
- ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने) के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिले।
- वे एक स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहते थे।
- उदारवादी एक ऐसा देश चाहते थे जो सभी धर्मों का सम्मान करे।
- उन्होंने वंशवादी शासकों की निरंकुश सत्ता का विरोध किया।
- वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते थे।
- उन्होंने शासकों एवं अधिकारियों से मुक्त एक प्रतिनिधित्व करने वाली, निर्वाचित संसदीय सरकार की माँग की।
प्रश्न 9.
1917 ई. की रूसी क्रान्ति में लेनिन की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
लेनिन बोल्शेविक दल का एक नेता था। वह समाज तथा देश में बदलाव के लिए क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता था। लेनिन मजदूरों में आर्थिक समानता लाना चाहता था। उसके विचार में संसदीय तौर-तरीके रूस जैसे देश में बदलाव नहीं ला सकते थे जहाँ लोकतंत्रात्मक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई संसद नहीं थी। अंततः बोल्शेविक रूस में 1917 ई. में एक सफल क्रान्ति ला सके और उन्होंने देश तथा समाज का ढाँचा पूरी तरह बदल दिया। उसने मजदूरों को 1917 की रूसी क्रांति के लिए एक हथियार के (UPBoardSolutions.com) रूप में संगठित किया। उसने युद्ध का अन्त करने और किसानों को भूमि स्थानान्तरित करने की कोशिश की। केरेंस्की की सरकार के पतन के बाद लेनिन विश्व की प्रथम कम्युनिस्ट सरकार का मुखिया बना।
प्रश्न 10.
1917 की रूसी क्रान्ति के प्रमुख कारण बताइए।
उत्तर:
रूस के उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर पर जर्मनी के नियंत्रण के कारण रूस का आयात बन्द हो चुका था। 1916 ई. तक रेलवे लाइनें टूट चुकी थीं। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते देश के स्वस्थ लोगों को युद्ध में लगा दिया गया था जिससे देश में मजदूरों की कमी हो गयी थी। रूस में रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गयी थी।
किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार को अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुण्ठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते और प्रायः जमींदारों की हत्या करते।
मजदूरों की स्थिति भी बहुत भयावह थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी सम्पत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन (UPBoardSolutions.com) मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कार्य घण्टों की कोई सीमा नहीं थी जिसके कारण उन्हें दिन में 12-15 घण्टे काम करना पड़ता था।
जार का निरंकुश शासन बिल्कुल निष्प्रभावी हो चुका था। वह एक स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट एवं दमनकारी शासक था जिसे देश के लोगों के हितों को कोई खयाल नहीं था।
![]()
प्रश्न 11.
1917 ई. की क्रान्ति के लिए रूस के पूँजीपति कहाँ तक उत्तरदायी थे?
उत्तर:
- सेना के पास अस्त्र-शस्त्र, खाद्य-सामग्री और यहाँ तक कि पहनने के लिए वर्दी तक की भी कमी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के दौरान भारी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। इसीलिए उन्हें युद्ध में भारी हार खानी पड़ी। इस प्रकार 1917 ई. की क्रांति लाने में रूस के पूँजीपतियों का भी योगदान था।
- पूँजीपति किसानों तथा मजदूरों को बुरी तरह शोषण कर रहे थे। युद्ध के दिनों में भी उनके सामने मुनाफा कमाने के सिवाय और कोई काम न था। इसी उद्देश्य से वे चीजों के दाम बढ़ाते चले गए।
- भ्रष्ट सेना अधिकारियों से मिलकर वे इतना अधिक मुनाफा कमाने लगे कि युद्ध के आठ महीनों में ही सेना को युद्ध सामग्री पहुँचानी असंभव हो गई।
प्रश्न 12.
रूस की 1905 ई. की क्रान्ति को 1917 ई. की क्रान्ति की जननी क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
9 जनवरी, 1905 ई. को रविवार के दिन मास्को में एक विशाल जुलूस रूसी शासक जार के महल की ओर अग्रसर था। आंदोलनकारी नेता जार को अपनी 11 सूत्रीय माँगों वाली एक याचिका देने जा रहे थे। जुलूस में शामिल लोग यह नारा लगा रहे थे कि “छोटे भगवान! हमें रोटी दो!” जार चाहता था कि रूस की जनता उसे भगवान की तरह पूजे। इसी कारण रूस के लोग उसे ‘छोटा भगवान’ कहते थे। जार के सैनिकों ने इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी जिसमें एक हजार के लगभग लोग वहीं मारे गए।
सेना ने 60 हजार के लगभग लोगों को बंदी बना लिया। इसीलिए 9 जनवरी, 1905 ई. का दिन रूस के इतिहास में लाल रविवार (खूनी रविवार) के नाम से जाना जाता है। उस समय तो प्रदर्शनकारियों को सेना ने बलपूर्वक दबा दिया किन्तु क्रान्ति की चिंगारी उनके भीतर सुलगती रही और 1917 ई. में एक क्रान्ति के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए 1905 ई. की क्रान्ति को 1917 ई. की क्रान्ति की जननी कहा जाता है।
प्रश्न 13.
प्रथम विश्व युद्ध का 1917 की रूसी क्रान्ति पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर:
प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ होने से पहले यूरोप में दो गुट सक्रिय थे। एक गुट में इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा रूस थे जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ होने के समय रूस अपने गुट का साथ देने के लिए युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन रूस के पास धन, सैन्य शक्ति और अस्त्र-शस्त्रों का अभाव था। ऐसे में रूसी सरकार ने किसानों को बलपूर्वक सेना में शामिल करके बड़ी संख्या में युद्ध के मैदान में भेज दिया। एक अनुमान के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए, 5 लाख के (UPBoardSolutions.com) लगभग घायल हुए तथा 20 लाख बन्दी बनाए गए। ऐसी विषम परिस्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों तथा पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावनाएँ पनपने लगीं। ये जनभावनाएँ आगे चलकर रूसी क्रान्ति का एक प्रमुख कारण बनीं।
प्रश्न 14.
किसानों की हीन दशा 1917 ई. की रूसी क्रान्ति हेतु उत्तरदायी थी।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
- किसानों पर करों को भारी बोझ होता था और वे सदा ऋण से दबे रहते थे। उन्हें दो वक्त भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। ऐसे में किसानों के पास सिवाय क्रान्ति के कोई चारा नहीं था। यही कारण था कि किसानों की हीन दशा 1917 ई. की क्रांति का मुख्य कारण बनी।
- 1861 ई. से पहले रूस में सामन्तवादी प्रथा थी। किसान भूमि-दासों के रूप में जमीनों को जोतते थे परन्तु उन्हें अपनी उपज का एक बड़ा भाग सामन्तों को देना पड़ता था।
- यद्यपि 1861 ई. में सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई थी परन्तु फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत छोटे-छोटे होते थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे।
![]()
प्रश्न 15.
अक्टूबर क्रान्ति के बाद रूस में गृह युद्ध का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हुआ?
उत्तर:
बोल्शेविकों द्वारा जमीन के पुनर्वितरण का आदेश देने पर रूसी सेना टूटने लगी। सैनिक और किसान जमीन के पुनर्वितरण के लिए घर जाना चाहते थे और अन्ततः उन्होंने सेना छोड़ना शुरू कर दिया। बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी, उनके नेता और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों के विद्रोह की निन्दा की। उनके नेता दक्षिण एशिया में चले गए और बोल्शेविकों (रेड्स) से लड़ने के (UPBoardSolutions.com) लिए टुकड़ियाँ एकत्र करने लगे। 1918 ई. और 1919 ई. के बाद ग्रीन्स (समाजवादी क्रांतिकारी) एवं ‘ह्वाइट्स’ (प्रो-जारीस्ट) ने अधिकतर रूसी साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया। फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेज एवं जापानी टुकड़ियों ने उनकी मदद की। ये सभी सेनाएँ भी रूस में बढ़ रहे समाजवाद से चिंतित थीं। इसलिए वहाँ इन टुकड़ियों एवं बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध हो गया। इसके परिणामस्वरूप लूटपाट, डकैती और भुखमरी आम हो गई।
प्रश्न 16.
प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 तथा 1916 ई. के बीच बुरी तरह पराजित हुई। 1917 ई. तक 70 लाख लोग युद्ध में मारे गए। पीछे हटते रूसी सैनिकों ने फसलों व इमारतों को इसलिए नष्ट कर दिया। जिससे शत्रु सेना को उस स्थान पर टिक पाना संभव न हों। फसलों और इमारतों के विनाश के परिणामस्वरूप 30 लाख से अधिक लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। इस स्थिति ने:आर और सरकार को अपने देश में लोकप्रिय बना दिया। युद्ध का उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
अनेक उद्योग बन्द हो गए। बाल्टिक सागर मार्ग पर जर्मनों का नियंत्रण होने के कारण रूस अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात न कर सका। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत हो गयी। 1916 ई. तक रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गयी। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस के औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से बेकार होने लगे। 1916 ई. तक रेलवे लाईंटूटने लगीं। सेहतमन्द लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया। परिणामस्वरूप मजदूरों की कमी हो गई और आवश्यक सामान बनाने वाली छोटी कार्यशालाओं को बन्द कर दिया गया। अनाज का एक बड़ा भाग सैनिकों के भोजन के लिए भेज दिया गया।
प्रश्न 17.
1905 ई. की रूसी क्रान्ति के पश्चात् जार ने रूस में क्या परिवर्तन किए?
उत्तर:
1905 ई. की क्रान्ति के पश्चात् जार द्वारा रूस के राजनैतिक परिवेश में निम्न महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए-
- जार ने प्रथम ड्यूमा को 75 दिन के अन्दर और पुनः निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को तीन माह के अन्दर बर्खास्त कर दिया। वह अपनी सत्ता पर किसी प्रकार की जवाबदेही अथवा अपनी शक्तियों में किसी तरह की कमी नहीं चाहता थी। उसने मतदान के नियम बदल डाले और उसने तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों तथा क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया।
- 1905 ई. की क्रान्ति के उपरान्त सभी समितियाँ एवं संगठन गैरकानूनी घोषित कर दिए गए।
- राजनैतिक दलों पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए गए।
प्रश्न 18.
बोल्शेविकों ने गृह युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को जारी रखने के लिए क्या किया?
उत्तर:
रूस में बोल्शेविक मजदूरों का बहुमत वाला समूह था जिसका नेता लेनिन था। बोल्शेविक समाज एवं देश में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी तरीकों को अपनाने में विश्वास करते थे।
बोल्शेविकों ने गृह युद्ध के दौरान उद्योगों तथा बैंकों को राष्ट्रीयकृत रखा। उन्होंने समाजीकरण की हुई भूमि पर किसानों को खेती करने दी। बोल्शेविकों ने जब्त की (UPBoardSolutions.com) गई भूमि के द्वारा यह दर्शाया कि सामूहिक कार्य क्या कर सकता है।
केन्द्रीयकृतं नियोजन की एक प्रक्रिया लागू की गई। कर्मचारियों ने यह आंका कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी और अगले 5 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। सभी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते थे।
केन्द्रीयकृत नियोजन से आर्थिक विकास को गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा (1929 से 1933 ई. के बीच में तेल, कोयले और इस्पात में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई)। नए औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
स्तालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का विवरण दीजिए।
उत्तर:
सोवियत रूस के कस्बे 1927-28 ई. तक अनाज की आपूर्ति में जबरदस्त कमी की समस्या से त्रस्त थे। अनाज की कमी की समस्या को दूर करने के लिए खेतों के सामूहिकीकरण का निर्णय सरकार द्वारा किया गया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि अनाज की यह कमी आंशिक रूप से खेतों के छोटे आकार के कारण है। 1917 ई. के बाद जमीन किसानों को दे दी गई। इन छोटे आकार के खेतों का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों (रूस के धनी किसान) का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित बड़े खेत बेनाना आवश्यक हो गया।
स्तालिन का विचार था कि कुलक (रूस के धनी किसान) अधिक फायदा पाने के लिए अनाज को नहीं बेच रहे थे। इसलिए स्तालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। 1929 ई. से सभी किसानों को सामूहिक खेत (कोलखोज) को जोतने के लिए विवश किया गया। ज्यादातर भूमि तथा (UPBoardSolutions.com) कृषि यंत्रों का स्वामित्व सामूहिक खेतों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसान भूमि पर काम करते तथा कोलखोज से होने वाला लाभ किसानों में बाँट दिया जाता था। यद्यपि स्तालिन की खेतों के सामूहिकीकरण की नीति किसानों में अलोकप्रिय थी और किसानों ने इसके विरोध में अपने पशुओं को मारना शुरू कर दिया।
फलस्वरूप 1929 से 1931 ई. के बीच पशुओं की संख्या एक तिहाई तक घट गयी। खेतों के सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को कठोर दण्ड दिया गया। स्तालिन सरकार ने कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति दी लेकिन ऐसे उत्पादकों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन तत्काल नहीं बढ़ा। 1930-33 ई. में खराब फसल के कारण भयंक़र अकाल पड़ा जिसमें चालीस लाख लोग मारे गए।
प्रश्न 2.
उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिन्होंने जार को सत्ता छोड़ने पर विवश किया?
उत्तर:
7 मार्च, 1917 ई. को रूस की क्रान्ति शुरू हुई। शुरू में रूस की महिलाओं ने देश की असहनीय परिस्थितियों के विरुद्ध एक जुलूस निकाला जिसमें वे रोटी की माँग कर रही थीं। शीघ्र ही सैनिक, कारीगर तथा अन्य लोग इन विरोध प्रदर्शनो में शामिल हो गए। इन क्रान्तिकारियों ने बन्दीगृहों पर धावा बोलकर कैदियों को स्वतन्त्र कर दिया। क्रांतिकारियों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। इन लोगों ने मास्को एवं सेंट (UPBoardSolutions.com) पीटर्सबर्ग पर अधिकार कर लिया। अंततः 15 मार्च, 1917 ई. को जार ने विवश होकर सत्ता का परित्याग कर दिया। राजकुमार ल्वोफ (केरेन्सकी) की देखरेख में पहली अस्थायी सरकार रूस में गठित की गयी।
निम्न कारण जार के पतन के लिए निश्चय ही उत्तरदायी थे-
- किसान वर्ग भूमि पर केवल खेती करने वालों का अधिकार चाहता था, परन्तु जार ऐसा करने को तैयार न था।
- कारीगर लोग कारखानों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, परन्तु जार ने ऐसा करना स्वीकार न किया।
- जार ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अनेक जातियों को अपना दास बना रखा था। ऐसी जातियाँ जार को सहयोग देने के लिए तैयार न थीं।
- बिना तैयारी के प्रथम विश्वयुद्ध में कूद पड़ने के कारण लाखों की संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। ऐसे वातावरण में लोग शांति चाहते थे जबकि जार युद्ध को जारी रखने की बात पर अड़ा हुआ था।
- देश में चारों ओर अकाल पड़ा था लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। जार लोगों की समस्या को नहीं सुलझा सका। अतः जार का शासन समाप्त हो गया और उसके राज्य का पतन हो गया।
![]()
प्रश्न 3.
रूसी क्रान्ति में लेनिन की भूमिका बताइए।
उत्तर:
- जार की साम्राज्यवादी नीति का दुष्परिणाम रूस को भुगतना पड़ा। निरन्तर युद्धों के कारण देश के धन एवं संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। देश का आर्थिक संकट गहराने लगा और जनता जार के विरुद्ध हो गयी।
- जार अपनी सुन्दर रानी जरीना के प्रभाव में था जबकि रानी जरीना पर रासपूतनिक नामक एक ढोंगी संत को प्रभाव था। यह ढोंगी संत दमन की नीति का पक्षपाती था। कहा जाता है कि यह संत एक गुण्डा था जो चोरी के अपराध में पकड़ा गया था। बाद में उसने साधु का वेश धारण कर लिया था। इतिहासकार रासपूतनिक को ‘होली डेविल के नाम से पुकारते हैं।
- 1905 ई. की क्रांति के कारण जार ने यह आश्वासन दिया था कि रूस में ड्यूमा अर्थात् पार्लियामेंट का निर्माण किया जाएगा परन्तु बाद में अपनी निरंकुशता के कारण उसने ड्यूमा को कोई काम नहीं करने दिया। वह इसके चुनाव में भी हस्तक्षेप करने लगा। पहली ड्यूमा (UPBoardSolutions.com) को उसने केवल ढाई महीने में ही भंग कर दिया। जार ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर रखा था जिसमें भाँति-भाँति के लोग रहते थे जो सदा उसके लिए कोई न-कोई समस्या खड़ी कर देते थे।
- रूस का जार निकोलस द्वितीय बिल्कुल उद्दण्ड और निरंकुश शासक था। 1905 ई. की क्रांति दबाने के बाद भी निकोलस द्वितीय की निरंकुशता बढ़ती ही गई। उसने गुप्तचर विभाग का कार्य बहुत तेज कर दिया। जिन लोगों का क्रांति से जरा-सा भी संबंध समझा गया, उनको या तो मार दिया गया या उन्हें बंदी बना लिया गया या फिर देश-निकाला दे दिया गया।
प्रश्न 4.
रूस की क्रान्ति के वैश्विक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
रूस की क्रान्ति का वैश्विक प्रभाव इस प्रकार है-
- रूस की देखा-देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा व मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की | पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू किया।
- जब राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई तो उसने विश्वभर के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए एक विशेष संस्था का निर्माण किया। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- इसी प्रकार अनेक सरकारों ने शिक्षा देने का कार्य चर्च से छीन लिया।
- पहले विश्वयुद्ध के बाद समाजवादी आंदोलन मोटे तौर पर दो भागों-सोशलिस्ट पार्टियों और कम्युनिस्ट पार्टियों में बँट गया। समाजवाद लाने की विधियों बल्कि समाजवाद की परिभाषा को लेकर भी उनके बीच अनेक मतभेद थे। इन मतभेदों के बावजूद अपने उदय (UPBoardSolutions.com) के कुछ ही दशकों के अन्दर समाजवाद सबसे अधिक स्वीकृत विचारधाराओं में से एक बन गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद समाजवादी आंदोलन के प्रभाव को फैलना कुछ सीमा तक रूसी क्रांति का परिणाम है।
- कम्युनिस्ट इंटरनेशनल (कोमिंटर्न), जिसका गठन पहली और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति की तर्ज पर किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतियों को प्रोत्साहन देने का साधन था। समाजवादी आन्दोलन में फूट पड़ गई। सोशलिस्ट पार्टियों के वामपंथी धड़ों ने अब स्वयं को कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में ढाल लिया। दुनिया के अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित थीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऐसा मंच बन गया जहाँ नीतियों पर विचार-विमर्श होते थे और दुनिया में लागू करने के लिए साझी नीतियाँ तय होती थीं। 1943 ई. में कोमिंटर्न को समाप्त कर दिया।
- क्रांति ने राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सभी क्षेत्रों में क्रान्ति ला दी।
- रूस की साम्यवादी सरकार को देखकर संसार के अन्य देशों, जैसे चीन व वियतनाम इत्यादि देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनीं।।
- रूस की क्रान्ति के बाद पूरे विश्व में पूँजीपतियों व मजदूर वर्ग में एक निरंतर संघर्ष-सा चल पड़ा।
- रूस में किसान व मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित हो जाने से इस वर्ग का सम्मान संसार के अन्य देशों में भी बढ़ा।
प्रश्न 5.
लेनिन की नयी आर्थिक नीति का विवेचन कीजिए।
उत्तर:
लेनिन की नयी आर्थिक नीति उसकी दूरदर्शिता का परिणाम थी जिसने रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया। नई आर्थिक नीति, 1921 ई. में लागू की गयी। इस नीति के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं-
- सरकारी फार्म स्थापित किए गए। इन फार्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य (रिसर्च) तथा नये-नये प्रयोग किए जाने लगे।
- भूमि की चकबंदी की गयी। इन बड़े फार्मों पर किसानों को नये यंत्र तथा अच्छी खाद-बीज आदि देकर मदद की गयी।
- लोगों को वेतन नकद दिया जाने लगा।
- युद्ध के समय साम्यवाद के अन्तर्गत (1917-1921) उठाए गए सभी कदमों को वापस ले लिया गया।
- अनाज और माल का निजी क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति फिर दे दी गई।
- कुछ उद्योगों में निजी प्रबंध स्वामित्व की छूट दी गई।
- रूस में बहुत बड़ी संख्या में सहकारी संघ या समितियाँ स्थापित किए गए।
- अकाल पीड़ितों की राहत के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किए गए।
प्रश्न 6.
रूस में 1905 ई. की क्रान्ति से पूर्व के घटनाक्रम का विवरण दीजिए।
उत्तर:
रूस में जार का शासन तानाशाही शासन का प्रतिरूप था। जार निकोलस द्वितीय एक भ्रष्ट, दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी शासक था। रूस में जार द्वारा जनसामान्य (UPBoardSolutions.com) की उपेक्षा ने ही लोगों की स्थिति को विपन्न बना दिया था। मजदूर और किसान आपस में विभाजित थे। किसान प्रायः लगाने देने से मना कर देते थे और कभी-कभी वे जमींदार की हत्या तक कर देते थे।
पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा किए गए लोकतांत्रिक प्रयोगों से प्रभावित होकर रूस के लोगों ने भी एक उत्तरदायी सरकार की माँग आरम्भ की, लेकिन जार ने उनकी माँग को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप उदार सुधारक भी क्रान्ति की बातें करने लगे।
सन् 1904 का वर्ष किसानों के लिए बहुत ही दुष्कर था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तथा मजदूरी 20 प्रतिशत तक घट गयी थी। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ा दी गयी। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर प्रतिदिन काम के घण्टों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्यस्थितियों में सुधार करने की माँगों को लेकर हड़ताल पर चले गए।
जनवरी, 1905 ई. में जोर से याचना करने के लिए एक रविवार को मजदूरों ने पादरी गैपॉन के नेतृत्व में एक शान्तिपूर्ण जुलूस निकाला। किन्तु जब यह जुलूस विंटर पैलेस पहुँचा तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप 100 से अधिक मजदूर इस हमले में मारे गए जबकि (UPBoardSolutions.com) इससे कहीं अधिक घायल हो गए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर दिया जिसे 1905 की क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। इसी कारण पूरे देश में हड़ताले
![]()
प्रश्न 7.
रूसी क्रान्ति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
रूसी क्रान्ति के प्रमुख कारण : 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्भिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। इनमें से ज्यादातर देश फ्रांस की भाँति गणतन्त्र थे और इंग्लैण्ड की भाँति संवैधानिक राजतंत्र। यूरोप के ज्यादातर देशों में प्राचीन सामंती अभिजात वर्ग के स्थान पर नवीन मध्यम वर्ग सत्तासीन हो गया था। लेकिन वह अभी भी पुरानी व्यवस्था में जी रहा था। इसी के चलते रूस में 1905 ई. और 1917 ई. में क्रान्ति घटित हुई। रूसी क्रान्ति के लिए निम्न परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं-
(1) विचारकों का प्रभाव- अनेक रूसी विचारक यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से बहुत प्रभावित हुए। वे उसी तरह के परिवर्तन रूस में भी चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों में जागृति लाने और मजदूरों में संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया। रूस की (UPBoardSolutions.com) तत्कालीन स्थितियों में एक नरमपंथी, जनतंत्रवादी अथवा सुधारक को भी क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के दौरान जनता के पास जाओ’ नामक एक आन्दोलन आरम्भ हुआ। यूरोप के उदार विचारों ने भी रूसी-क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया।
भौतिक क्रांति से पहले रूसी जनता के विचारों में क्रांति हुई। जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पश्चिम के उदार विचारकों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। विभिन्न रूसी लेखकों जैसे टालस्टाय, टर्जने आदि ने नवयुवकों के विचारों में क्रांति पैदा कर दी और वे पश्चिमी देशों के लोगों को प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों की माँग करने लगे। जार ने जब उन्हें ठुकराने की कोशिश की तो उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया।
(2) 1904-05 ई. में रूस-जापान युद्ध- 1904-05 ई. के रूसी-जापानी युद्ध में रूस की हार हुई। छोटे से देश से हारने के कारण जनता जार के शासन की विरोधी बन गई; क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि इस हार का
एकमात्र कारण जार की निर्बल और अयोग्य सरकार है जो युद्ध का ठीक प्रकार संचालन करने में असफल रही है।
(3) प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति- प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना की कई मोर्चे पर पराजय हुई। इस युद्ध में रूस के 60 लाख सैनिक मारे गए। रूस के लोग युद्ध को चालू रखने के पक्ष में नहीं थे। लगभग समस्त देशवासियों और विशेषकर सैनिकों में युद्ध को लेकर आक्रोश व्याप्त था।
(4) निरंकुश राजतंत्र- रूस की राजनैतिक स्थिति अक्टूबर क्रान्ति से बहुत अच्छी नहीं थी। चूँकि रूस में लम्बे समय से जार का निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, अकुशल और शोषक शासन अस्तित्व में था, ऐसे में रूस में क्रान्ति का घटित होना अवश्यम्भावी नहीं था। क्रांति से पूर्व रूस में शासन पर भ्रष्ट जमींदारों, शाही परिवार के लोगों, अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों का प्रभुत्व था। कहने को तो रूस का साम्राज्य बहुत बड़ा था लेकिन इसमें गैररूसी जनता पर और भी अधिक अत्याचार होते थे।
जार को शेष जनता की भावनाओं का कोई आदर नहीं था। वस्तुतः शासकों व शासितों के मध्य अन्तर निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था। अतः जनता में असंतोष की सभी सीमाएँ पार हो गई थीं। रूस के जार पूरी तरह निरंकुश व स्वेच्छाचारी थे। उन्होंने समय-समय पर जो परामर्शदात्री सभाएँ बनाईं, उनके विचारों को मानने के लिए वे बाध्य नहीं थे। जापान से परास्त हो जाने के बाद निकोलस द्वितीय को ड्यूमा (UPBoardSolutions.com) नामक संसद के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा किन्तु वह वास्तव में जनता तथा विशेषतः समाज के दुर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। दूसरे
इसकी शक्तियाँ सीमित थीं। सम्राट इसके निर्णय से बँधा हुआ नहीं था।
वह पूर्ववत् निरंकुश शासक बना रहा। जब कभी जार के शासन के विरुद्ध जन-आंदोलन उठे, उन्हें निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया। जार दैवी सिद्धान्त में विश्वास रखती था। वह और उसकी बुद्धिहीन पत्नी भोग-विलास में डूबे थे। जनसाधारण को कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।
(5) किसानों की विपन्न दशा- रूस में किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। रूस में 1861 ई. से पहले। सामन्तवादी व्यवस्था अस्तित्व में थी। अधिकांश किसान भूमि दासों या सर्फ के रूप में जमीन जोता करते थे। उन्हें अपनी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामंतों को देना पड़ता था। यद्यपि 1861 ई. में सामंत-प्रथा समाप्त कर दी गई तो भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे (UPBoardSolutions.com) होते थे जिने पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उन पर लगे करों को बोझ भारी थी इसलिए वे सदा ऋण से दबे रहते थे। सच तो यह है कि उन्हें दो समय का भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। रूस में जमीन के लिए किसानों की भूख असंतोष का एक प्रबल सामाजिक कारण था।
(6) श्रमिकों की विपन्न दशा- औद्योगिक क्रान्ति के कारण रूस में अनेक उद्योगों की स्थापना की गयी थी, जिनमें लाखों मजदूर काम करते थे किन्तु मजदूरों की आर्थिक स्थिति और उनके कार्यस्थल की दशाएँ अत्यन्त शोचनीय थीं। ऐसी दयनीय स्थिति से बचने के लिए मजदूर एक होने लगे। उन्होंने श्रम संघों का निर्माण शुरू किया। परन्तु पूँजीपति व उनके इशारों पर चलने वाली सरकार ने 1900 ई. में श्रम संघ बनाने एवं हड़ताल करने पर रोक लगा दी। उन्हें न तो कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही उन्हें सुधारों की कोई उम्मीद थी।
(7) 1905 ई. की क्रान्ति- 9 जनवरी, 1905 को रविवार के दिन मास्को में जनसाधारण ने अपनी 11 सूत्रीय माँगों के साथ एक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य इन 11 सूत्रीय माँगों को जार के महल तक जाकर उसे जार को सौंपना था। “छोटे भगवान! हमें रोटी दो।” के नारे के साथ ये लोग जार के महल की ओर बढ़ रहे थे, किन्तु जार ने इनसे बात करना तो दूर इन पर गोली चलवा दी। लगभग 1,000 प्रदर्शनकारी मारे गए तथा 60,000 गिरफ्तार कर लिए गए। रूस की सड़कों पर इस दिन बहुत रक्तपात हुआ। इसीलिए 9 जनवरी, 1905 ई. का रविवार का दिन रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक इतिहासकारों की राय है कि यद्यपि 1905 ई. की क्रांति को कुचलने में जार कामयाब रहा लेकिन इस क्रांति ने अक्टूबर, 1917 ई. की क्रांति के लिए उचित वातावरण तैयार करने में अहम् भूमिका अदा की। इस दिन हुए हत्याकांड से सारे रूस में रोष फैल गया। क्रांतिकारियों के (UPBoardSolutions.com) समर्थन में जगह-जगह बन्द आयोजित किए गए और हड़ताले हुईं। इस क्रांति के कारण शिक्षित वर्ग के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। इसीलिए 1905 ई. की क्रांति को कई बार 1917 ई. की क्रांति की जननी भी कहा जाता है।
Hope given UP Board Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 2 are helpful to complete your homework.
If you have any doubts, please comment below. UP Board Solutions try to provide online tutoring for you.