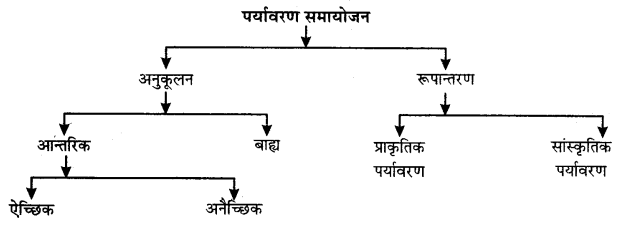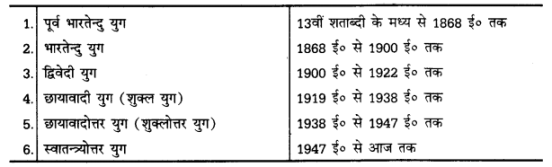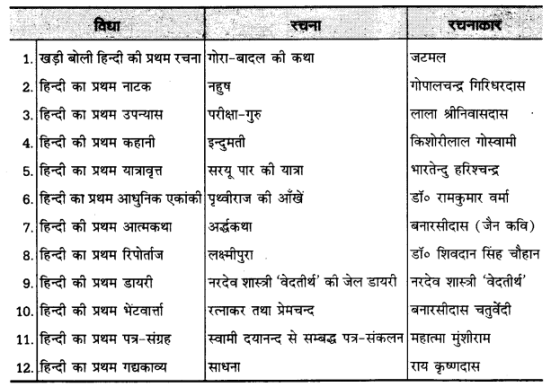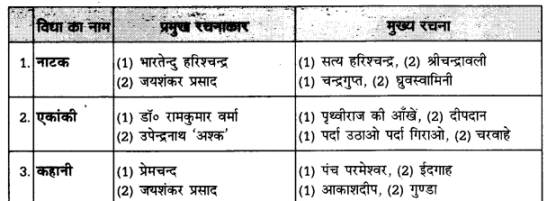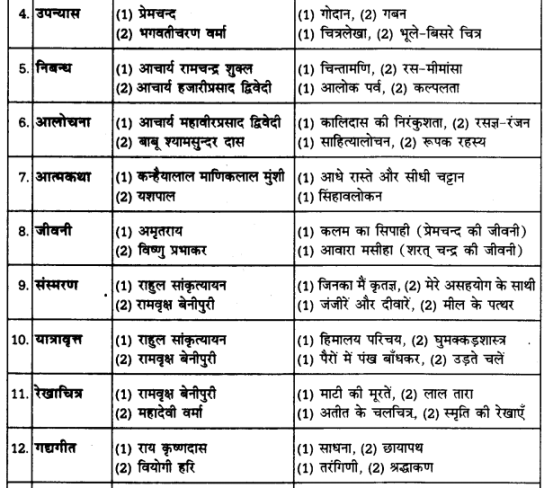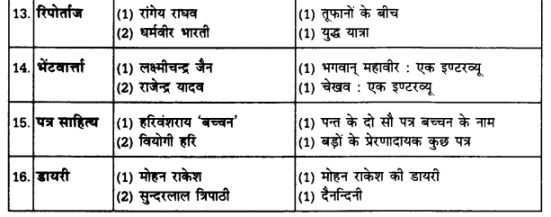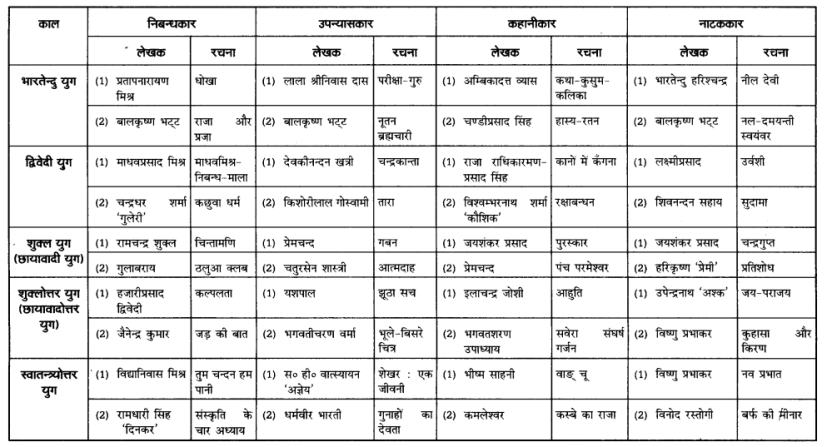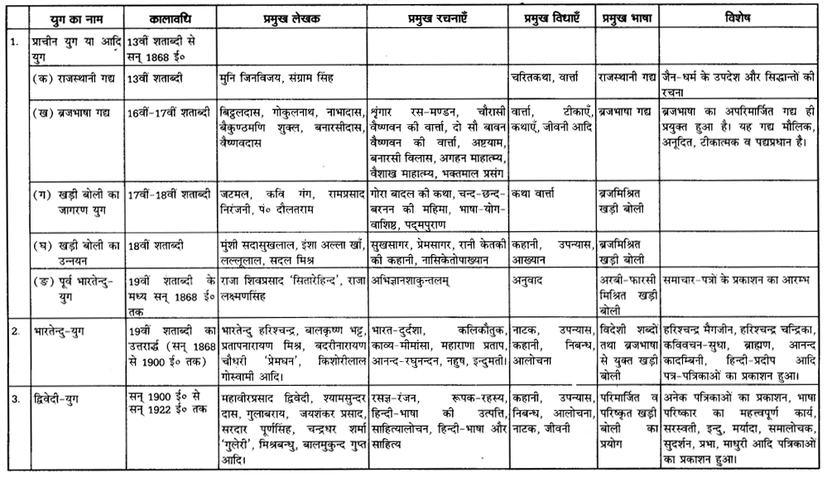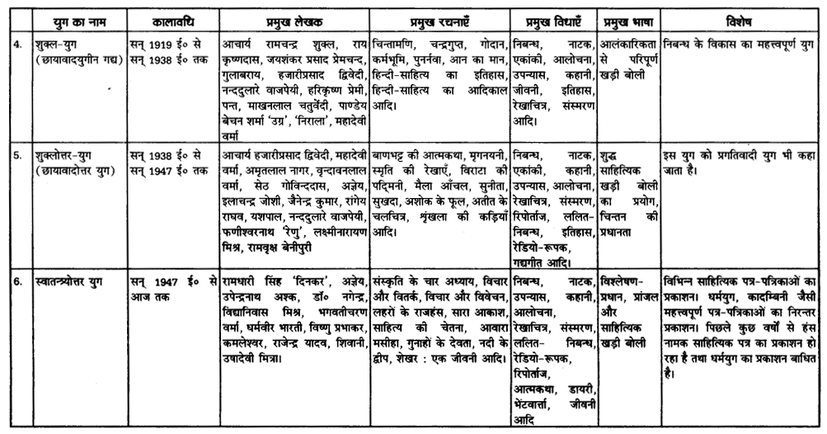UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी) are part of UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi . Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 11 |
| Subject | Sahityik Hindi |
| Chapter | Chapter 2 |
| Chapter Name | सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी) |
| Number of Questions | 9 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी)
प्रश्न 1:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य का कथानक (कथावस्तु) संक्षेप में लिखिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में वर्णित अत्यधिक मार्मिक प्रसंग का निरूपण कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर द्रौपदी और दुःशासन के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए।
या
‘सत्य की जीत’ में धृतराष्ट्र ने लोकमंगल की जिस नीति की उदघोषणा की है, उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
या
‘सत्य की जीत’ के आधार पर दुःशासन एवं विकर्ण के शस्त्र एवं शास्त्र सम्बन्धी विचारों की सम्यक विवेचना कीजिए।
या
“शस्त्र को सर्वस्व मानना विनाश का मूल है।” यह बात ‘सत्य की जीत’ में किस प्रकार अभिव्यक्त की गयी है ?
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
प्रस्तुत खण्डकाव्य की कथा द्रौपदी के चीर-हरण से सम्बद्ध है। यह कथानक महाभारत के सभापर्व में द्यूतक्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यन्त लघुकाव्य है, जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान सन्दर्भो में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संक्षेप में अग्रवत् है–
दुर्योधन पाण्डवों को द्यूतक्रीड़ा के लिए आमन्त्रित करता है। पाण्डव उसके निमन्त्रण को स्वीकार कर लेते हैं। युधिष्ठिर जुए में निरन्तर हारते रहते हैं और अन्त में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात् द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दुर्योधन दु:शासन को आदेश देता है कि वह बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में लाये। दु:शासन राजमहल से द्रौपदी के केश खींचते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंहनी के संमान गरजती हुई दुःशासन को ललकारती है। द्रौपदी की गर्जना से पूरा राजमहल हिल जाता है और समस्त सभासद स्तब्ध रह जाते हैं-
ध्वंस विध्वंस प्रलय का दृश्य, भयंकर भीषण हा-हाकार।
मचाने आयी हूँ रे आज, खोल दे राजमहल का द्वार ॥
इसके पश्चात् द्रौपदी और दु:शासन में नारी पर पुरुष द्वारा किये गये अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उनके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय-अन्याय आदि विषयों पर वाद-विवाद होता है। अहंकारी दु:शासन भी क्रोध में आ जाता है। ‘भरी सभा में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं तो मुझे दाँव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है ? द्रौपदी के इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित होते हैं। वह युधिष्ठिर की सरलता और दुर्योधन आदि कौरवों की कुटिलता का भी रहस्य प्रकट करती है। वह कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर छले गये हैं; अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दें कि क्या वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार करते हैं ?
कहता है कि यदि शास्त्र-बल से शस्त्र-बल ऊँचा और महत्त्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध . हो जाएगा; क्योंकि शस्त्र-बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुते तर्क पर धर्मपूर्वक और न्यायसंगत निर्णय होना चाहिए। वह कहता है कि द्रौपदी किसी प्रकार भी कौरवों द्वारा जीती हुई नहीं है।
किन्तु कौरव ‘विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। दुःशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने सम्पूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। वह कहती है कि मैं किसी प्रकार भी विजित नहीं हैं और उसके प्राण रहते उसे कोई भी निर्वस्त्र नहीं कर सकता। यह सुनकर मदान्ध दु:शासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए पुन: हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके दुर्गा-जैसे तेजोद्दीप्त भयंकर रौद्र-रूप को देख दुःशासन घबरा जाता है और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है।
द्रौपदी कौरवों को पुनः चीर-हरण करने के लिए ललकारती है। सभी सभासद द्रौपदी के सत्य, तेज और सतीत्व के आगे निस्तेज हो जाते हैं। वे सभी कौरवों की निन्दा तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। मेदान्ध दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण आदि को द्रौपदी पुन: ललकारती हुई कहती है-
और तुमने देखा यह स्वयं, कि होते जिधर सत्य और न्याय ।
जीत होती उनकी ही सदा, समय चाहे कितना लग जाय ॥
वहाँ उपस्थित सभी सभासद कौरवों की निन्दा करते हैं; क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि पाण्डवों के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।
अन्त में धृतराष्ट्र उठते हैं और पाण्डवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते। हैं। इसके साथ ही चे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानवं-जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे पाण्डवों की कल्याण-कामना करते हुए कहते हैं-
तुम्हारे साथ तुम्हारी सत्य, शक्ति श्रद्धा, सेवा औ’ कर्म ।
यही जीवन के शाश्वत मूल्य, इन्हीं पर टिका मनुज का धर्म ॥
इन्हीं को लेकर दृढ़ अवलम्ब, चल रहे हो तुम पथ पर अभय ।
तुम्हारा गौरवपूर्ण भविष्य, प्राप्त होगी पग-पग पर विजय ॥
धृतराष्ट्र द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हैं। वे उसके प्रति किये गये दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा माँगते हैं। तथा कहते हैं-
जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत।
तुम्हारे यश-गौरव के दिग्-दिगन्त में गूंजेंगे स्वर, गीत ॥
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस खण्डकाव्य की कथा द्रौपदी के चीरहरण की अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी बनाया है और युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दुहराया है।
प्रश्न 2:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ की कथावस्तु की समीक्षा कीजिए।
या
“वस्तु-सौष्ठव एवं संगठन की दृष्टि से ‘सत्य की जीत’ एक सफल खण्डकाव्य है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए।
या
खण्डकाव्य की दृष्टि से ‘सत्य की जीत’ काव्य की समीक्षा (आलोचना) कीजिए।
या
“सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के रचना-कौशल पर प्रकाश डालिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की पात्र-योजना अथवा पात्रों की प्रतीकात्मकता पर अपनी दृष्टि डालिए।
उत्तर:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य कथा-संगठन एवं उसके रचना-शिल्प के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है
(1) प्रसिद्ध पौराणिक घटना पर आधारित – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु द्रौपदी के चीर-हरण’ की पौराणिक घटना पर आधारित है। महाभारत में वर्णित यह मार्मिक प्रसंग सभी युगों में विद्वानों द्वारा विवाद एवं निन्दात्मक समस्या का विषय बना रहा है। तत्कालीन युग में विदुर ने नारी के इस अपमान को भीषण विनाश का पूर्व संकेत माना था और अधिकांश समालोचकों के अनुसार महाभारत के युद्ध का कारण भी प्रमुख रूप से यही था। पाण्डवों को तत्कालीन समाज का भावनात्मक समर्थन भी इसी कारण मिला था। कवि ने इसी मार्मिक घटना को अपने खण्डकाव्य की कथावस्तु बनाया है।
(2) कथावस्तु का संगठन – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने संवादों के माध्यम से कथा का संगठन किया है। प्रसंग लघु होने के कारण संवाद-सूत्र में व्यक्त की गयी इस कथा का संगठन अत्यन्त उत्तम कोटि का है। कवि ने वातावरण, मनोवेग, आक्रोश आदि की अभिव्यक्ति जिन संवादों द्वारा की है, वह अपनी व्यंजना में पूर्णतया सफल रहे हैं। कथावस्तु में केवल राजसभा का एक दृश्य सामने आता है, किन्तु नाटकीय आरम्भ एवं कौतूहलपूर्ण मोड़ों से गुजरती हुई कथावस्तु स्वाभाविक रूप में तथा त्वरित गति से अपनी सीमा की ओर बढ़ी
(3) कथावस्तु की लघुता में विशालता – ‘सत्य की जीत’ का कथा-प्रसंग अत्यन्त लघु है। कवि ने द्रौपदी के चीर-हरण के प्रसंग पर अपने खण्डकाव्य की कथावस्तु-योजना तैयार की है। इस एक घटना को लेकर कवि ने प्रस्तुत खण्डकाव्य में विशद वस्तु-योजना की है, जिसमें महाभारत काल के साथ-साथ वर्तमान युग के समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश की उद्घोषणा हुई है ।
पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ, बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग।
चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा पूरा.यह सर्ग।
(4) मौलिकता – यद्यपि ‘सत्य की जीत की कथा महाभारत की चीर-हरण घटना पर आधारित है, किन्तु कवि ने उसके प्रस्तुतीकरण में वर्तमान नारी की दशा को प्रस्तुत किया है और कुछ मौलिक परिवर्तन भी किये हैं। वे द्रौपदी के वस्त्र को श्रीकृष्ण द्वारा बढ़ाया जाता हुआ नहीं दिखाते, वरन् स्वयं द्रौपदी को ही अपने आत्मबल के प्रयोग के द्वारा दुःशासन को रोकते हुए दिखाते हैं। माहेश्वरी जी ने इस प्रसंग को स्वाभाविक एवं बुद्धिगम्य बना दिया है।
(5) देशकाल एवं वातावरण – इस खण्डकाव्य में महाभारतकालीन देशकाल एवं वातावरण का अनुभव अत्यन्त कुशलता से कराया गया है। दृश्य तो एक ही है, किन्तु पात्रों के संवाद एवं उनकी छवि के अंकन से इस देशकाल एवं वातावरण का पूर्ण स्वरूप सामने आ जाता है।
(6) नाटकीयती अथवा संवाद-योजना – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने कथोपकथनों के द्वारा कथा को प्रस्तुत किया है। इसके संवाद सशक्त, पात्रानुकूल तथा कथा-सूत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। कवि के इस प्रयास से काव्य में नाटकीयता का समावेश हो गया है, जिस कारण ‘सत्य की जीत काव्य अधिक आकर्षक बन गया है। द्रौपदी का यह संवाद उसकी निडर मनोवृत्ति का परिचायक हैं
अरे ओ दुर्योधन निर्लज्ज, करता यों बढ़-बढ़कर बात।
बाल बाँकी कर पाया नहीं, तुम्हारा वीर विश्वविख्यात ।।
(7) सुसम्बद्धता – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु पात्रों के कथोपकथनों की कड़ियों से सुसम्बद्ध हैं। कवि की कल्पना-शक्ति, अद्भुत प्रस्तुतीकरण और प्रबन्धात्मकता सभी सराहनीय हैं। कथा में आदि से अन्त तक कहीं भी अव्यवस्था नहीं आयी है। इस प्रकार समस्त कथावस्तु सुसम्बद्ध एवं सुव्यवस्थित है।
(8) खण्डकाव्य का सन्देश और उद्देश्य – प्रस्तुत खण्डकाव्य में कवि ने पात्रों के कथोपकथनों तथा तर्कवितर्क द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि असत्य, क्रूरता, अहंकार, अन्याय और अत्याचार की पराजय अवश्य होती है। कवि का उद्देश्य प्रस्तुत खण्डकाव्य की कथा के द्वारा नारी-जागरण एवं शस्त्रों के भण्डारण के विरुद्ध मानवतावादी भावना को स्वर देना है। राष्ट्र या समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी इस खण्डकाव्य की कथावस्तु का उद्देश्य है।
(9) पात्रों की प्रतीकात्मकता – इस खण्डकाव्य में प्रस्तुत किये गये सभी पात्रों का प्रतीकात्मक महत्त्व है। द्रौपदी सत्य, न्याय, धर्म आदि के गुणों की पुंज एवं अपने अधिकारों के लिए सजग और प्रगतिशील नारी को प्रतीक है। दु:शासन और दुर्योधन अनैतिकता एवं हिंसावृत्ति के प्रतीक हैं। पाण्डवों की प्रतीकात्मकता निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है
युधिष्ठिर सत्य, भीम हैं शक्ति, कर्म के अर्जुन हैं अवतार।
नकुल श्रद्धा, सेवा सहदेव, विश्व के हैं ये मूलाधार ॥
(10) पात्रों का चयन एवं समायोजन – कवि ने इस खण्डकाव्य की कथा-योजना में महाभारतकालीन उन्हीं प्रमुख पात्रों को लिया है, जिनका द्रौपदी के चीर-हरण प्रसंग में उपयोग किया जा सकता था। नवीनता यह है कि इन पात्रों में श्रीकृष्ण को किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रमुख पात्र द्रौपदी एवं दु:शासन हैं। अन्य पात्रों का उल्लेख केवल वातावरण एवं प्रसंग को उद्दीपन प्रदान करने के लिए हुआ है। पात्रों को चरित्र-चित्रण स्वाभाविक है और उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति की बड़ी सुन्दर अभिव्यंजना हुई है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वस्तु-संगठन की दृष्टि से खण्डकाव्य की कथा लघु होनी चाहिए, नायक या नायिका में उदात्त-गुणों का समावेश होना चाहिए और कथा का विस्तार क्रमिक एवं उद्देश्य आदर्शों की स्थापना होना चाहिए। इन सभी विशेषताओं का समावेश इस खण्डकाव्य में सफलतापूर्वक किया गया है; अतः यह एक सफल खण्डकाव्य है।।
प्रश्न 3:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में निहित सन्देश (उद्देश्य) को स्पष्ट कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ में प्रतिपादित आदर्शों का सोदाहरण विवेचन कीजिए।
या
” ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने मानवीय आदर्श एवं शाश्वत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, इस कथन की पुष्टि कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ की प्रमुख विचारधारा पर प्रकाश डालिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि की सफलता पर प्रकाश डालिए।
या
‘सत्य की जीत’ के प्रमुख विचार-बिन्दुओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
या
” ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु पौराणिक होते हुए भी आधुनिक विचारधारा की पोषक है,” उद्धरण देकर सिद्ध कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ में जिन उदात्त जीवन-मूल्यों का चित्रण किया गया है, उन्हें सोदाहरण समझाइए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य से समाज को क्या सन्देश मिलता है ? ‘सत्य की जीत’ शीर्षक की सार्थकता को प्रमाणित कीजिए। ‘सत्य की जीत के आधार पर ‘जीओ और जीने दो’ की समीक्षा कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में नारी विषयक अवधारणा का चित्रण कीजिए।
उत्तर:
सत्य की जीत’ शीर्षक से स्वतः स्पष्ट है कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी प्रस्तुत खण्डकाव्य में असत्य पर सत्य की विजय प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसे खण्डकाव्य में द्रौपदी के चीर-हरण का प्रसंग वर्णित किया गया है, किन्तु इसमें कथा का रूप सर्वथा मौलिक है। अत्याचारियों के दमन को द्रौपदी झुककर स्वीकार नहीं करती, वरन् वह पूर्ण आत्म-बलं से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करती है। उसकी पक्ष सत्य एवं न्याय का पक्ष है। अन्ततः उसकी ही जीत होती है और पूरी राजसभा उसके पक्ष में हो जाती है।
प्रस्तुत खण्डकाव्य में कवि का उद्देश्य असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाना है तथा खण्डकाव्य का मुख्य आध्यात्मिक भाव भी यही है। इस दृष्टिकोण से इसे खण्डकाव्य का यह शीर्षक पूर्णरूप से उपयुक्त और सार्थक है। इस खण्डकाव्य में निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन हुआ है
(1) नैतिक मानव-मूल्यों की स्थापना – ‘सत्य की जीत’ में कवि ने दुःशासन और दुर्योधन के छल-कपट, दम्भ, ईष्र्या, अनाचार, शस्त्र-बल, परपीड़न आदि की पराजय दिखाकर उन पर सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, मैत्री, करुणा, श्रद्धा आदि शाश्वत मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा की है और कहा है
जहाँ है सत्य, जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय, वहाँ है जीत।
कवि का विचार है कि मानव को भौतिकवाद के गर्त से नैतिक मूल्यों की स्थापना के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
(2) नारी की प्रतिष्ठा – कवि ने प्रस्तुत खण्डकाव्य में द्रौपदी को श्रृंगार व कोमलता की परम्परागत मूर्ति के रूप में नहीं, वरन् दुर्गा के नव रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो अपने सतीत्व और मर्यादा की रक्षा के लिए चण्डी और दुर्गा भी बन जाती है। यही कारण है कि भारत में नारी की शक्ति को दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। द्रौपदी दुःशासन से स्पष्ट कह देती है कि नारी पुरुष की सम्पत्ति या भोग्या नहीं है। उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। पुरुष और नारी के सहयोग से ही विश्व का मंगल सम्भव है
पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ, बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग।
चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा पूरा यह सर्ग ॥
(3) प्रजातान्त्रिक भावना का प्रतिपादन – प्रस्तुत खण्डकाव्य का सन्देश है कि हम प्रजातान्त्रिक भावनाओं का आदर करें। किसी एक व्यक्ति की निरंकुश नीति को अनाचार की छूट न दें। राजसभा में द्रौपदी के प्रश्न पर जहाँ दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं वहीं धृतराष्ट्र अपना निर्णय देते समय जन-भावनाओं की अवहेलना भी नहीं करते।
(4) स्वार्थ और ईष्र्या का उन्मूलन – आज का मनुष्य ईर्ष्या व स्वार्थ के चंगुल में फंसा हुआ है। ईर्ष्या और स्वार्थ संघर्ष को जन्म देते हैं। इनके वशीभूत होकर व्यक्ति सब कुछ कर बैठता है-इसे कवि ने कौरवों द्वारा द्रौपदी के चीर-हरण की घटना से व्यक्त किया है। दुर्योधन पाण्डवों से ईर्ष्या रखता है, जिसके कारण वह उन्हें द्यूतक्रीड़ा में हराकर उन्हें नीचा दिखाने तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उन्हें अपमानित करना चाहता है। कवि स्वार्थ और ईर्ष्या को पतन का कारण सिद्ध करता है और उनके स्थान पर मैत्री, त्याग और सेवा जैसे लोकमंगलकारी भावों को प्रतिष्ठित करना चाहता है।
(5) सहयोग, सह-अस्तित्व और विश्व-बन्धुत्व का सन्देश – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने आज के युग के अनुरूप यह सन्देश दिया है कि सहयोग और सह-अस्तित्व के विकास से ही विश्व-कल्याण होगा–जियें हम और जियें सब लोग। इससे सत्य, न्याय, मैत्री, करुणा और सदाचार को बल मिलेगा, जिससे व्यक्ति को समस्त संसार एक कुटुम्ब की भाँति प्रतीत होने लगेगा।
(6) शान्ति की कामना – प्रस्तुत खण्डकाव्य में कवि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। वह शस्त्र बल पर सत्य, न्याय और शास्त्र की विजय दिखलाता है। धृतराष्ट्र भी शस्त्रों का प्रयोग स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए किये जाने पर बल देते हैं
किये हैं जितने भी एकत्र, शस्त्र तुमने, उनका उपयोग।
युद्ध के हित नहीं, शान्ति हित करो, यही है उनका स्वत्व प्रयोग।
(7) निरंकुशवाद के दोषों का प्रकाशन – प्रस्तुत खण्डकाव्य के द्वारा कवि यह बताना चाहता है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो वह अनैतिक कार्य करने में भी कोई संकोच नहीं करती। ऐसे राज्य में विवेक पूर्णतया कुण्ठित हो जाता है। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि भी दुर्योधन की सत्ता की निरंकुशता के आगे हतप्रभ हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में भारतीय शाश्वत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा की गयी है। इस खण्डकाव्य के द्वारा कंवि अपने पाठकों को सदाचारपूर्ण जीवन की प्रेरणा देना चाहता है। वह उन्नत मानवीय जीवन का सन्देश देता हैं। धृतराष्ट्र की उदारतापूर्ण इस घोषणा में काव्य का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है
नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जियें हम और जियें सब लोग।
बाँटकर आपस में मिले सभी, धरा का करें बराबर भोगे॥
प्रश्न 4:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
” ‘सत्य की जीत’ में द्रौपदी के चरित्र में वर्तमान युग के नारी-जागरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।” स्पष्ट कीजिए।
या
“सत्य की जीत’ के किसी मुख्य पात्र की चरित्रगत विशेषताएँ लिखिए।
या
‘सत्य की जीत’ के आधार पर द्रौपदी के चरित्र-चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
या
“नारी अबला नहीं, शक्तिरूपा है।” द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ में कवि ने द्रौपदी के चरित्र में जो नवीनताएँ प्रस्तुत की हैं, उनका उदघाटन करते हुए उसके चरित्र-वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए।
या
‘सत्य की जीत के आधार पर द्रौपदी के संघर्षमय जीवन का चित्रण कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ की नायिका द्रौपदी के चरित्र में समाविष्ट मानवीय आदर्शों का विश्लेषण कीजिए।
या
द्रौपदी का पक्ष सत्य और न्याय का पक्ष है। इस बात को सिद्ध कीजिए।
उत्तर:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं-
(1) नायिका: द्रौपदी ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की नायिका है। सम्पूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। वह राजा द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन तथा युधिष्ठिर सहित पाँचों पाण्डवों की पत्नी है। ‘सत्य की जीत खण्डकाव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी वह बड़े आत्मविश्वास से दु:शासन को अपना परिचय देती हुई कहती है
जानता नहीं कि मैं हूँ कौन ? द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन।
पाण्डुकुल वधू भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर को कब रे यह सहन॥
(2) स्वाभिमानिनी सबला – द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपना अपमान नारी-जाति का अपमान समझती है। और वह इसे सहन नहीं करती। ‘सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भाँति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। यह द्रौपदी तो अन्यायी, अधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष व विरोध करने वाली है। इस प्रकार उसका निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है
समझकर एकाकी, निशंक, दिया मेरे केशों को खींच।
रक्त का पैंट पिये मैं मौन, आ गयी भरी सभा के बीच ॥
इसलिए नहीं कि थी असहाय, एक अबला रमणी का रूप।
किन्तु था नहीं राज-दरबार, देखने मेरा भैरव-रूप ।।
(3) विवेकशीला – द्रौपदी पुरुष के पीछे-पीछे आँख बन्द कर चलने वाली नारी नहीं, वरन् विवेक से कार्य करने वाली नारी है। आज की नारी की भाँति वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सजग है। द्रौपदी की स्पष्ट मान्यता है कि नारी में अपार शक्ति और आत्मबल विद्यमान है। पुरुष स्वयं को संसार में सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न समझता है, किन्तु द्रौपदी इस अहंकारपूर्ण मान्यता का खण्डन करती हुई कहती है
नहीं कलिंका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई-मुई-सा गात !
पुरुष की है यह कोरी भूल, उसी के अहंकार की बात ॥
वह केवल दुःशासन ही नहीं वरन् अपने पति को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर स्पष्टीकरण माँगती है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जुए में स्वयं को हारने वाले युधिष्ठिर को मुझे दाँव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।-
द्रौपदी के वचन सुनकर सम्पूर्ण सभा, स्तब्ध और किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाती है और द्रौपदी के तर्को पर न्यायपूर्वक विचार करने के लिए विवशं हो जाती है। द्रौपदी के ये कथन उसकी वाक्पटुता एवं योग्यता के परिचायक हैं।
(4) साध्वी – द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ-साथ सत्य, शील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं।
द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी न्याय सत्य साकार।
इसी से आज सभी से प्राप्त, उसे बल सहानुभूति अपार ॥
(5) ओजस्विनी – ‘सत्य की जीत’ की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। वह अपना अपमान होने पर सिंहनी की भाँति दहाड़ती है
सिंहनी ने कर निडर दहाड़, कर दिया मौन सभा को भंग।
दुःशासन द्वारा केश खींचने के बाद वह रौद्र-रूप धारण कर लेती है। कवि कहती है
खुली वेणी के लम्बे केश, पीठ पर लहराये बन काल।।
उगलते ज्यों विष कालिया नाग, खोलकर मृत्यु-कणों का जाल ।
(6) सत्य, न्याय और धर्म की एकनिष्ठ साधिका – द्रौपदी सत्य और न्याय की अजेय शक्ति और असत्य तथा अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचन बहुत संयत शब्दों में करती हुई कहती है
सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिये मैं साथ।
अरे, वह कौन विश्व में शक्ति, उठा सकती जो मुझ पर हाथ॥
(7) नारी-जाति की पक्षधर – ‘सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। भारतीय संस्कृति के आधार वेद हैं और वेदों के अनुसार आदर्श नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्म-सम्मान, सत्य, धर्म, व्यवहारकुशलता, वाक्पटुता, सदाचार आदि गुण विद्यमान होते हैं। द्रौपदी में भी ये सभी गुण विद्यमान हैं। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभा में गरज उठती है
मौन हो जा मैं सह सकतीन, कभी भी नारी का अपमान।
दिखा देंगी तुझको अभी, गरजती आँखों का तूफान ।।
द्रौपदी को पता है कि नारी में अपार शक्ति-सामर्थ्य, बुद्धि और शील विद्यमान हैं। नारी ही मानव-जाति के सृजन की अक्षय स्रोत है। वह नारी-जाति को पुरुष के आगे हीन सिद्ध नहीं होने देती है। नारी की गरिमा का वर्णन करती हुई वह कहती है
पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण।
(8) वीरांगनां – वह पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली असहाय अबला नहीं वरन् चुनौती देकर दण्ड देने को कटिबद्ध है
अरे ओ दुःशासन निर्लज्ज, देख तू नारी को भी क्रोध ।
किसे कहते उसका अपमान, कराऊँगी मैं उसका बोध ॥
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पाण्डव-कुलवधू, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव- सम्पन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती-साध्वी, नारीत्व के स्वाभिमान से मण्डित एवं नारी जाति का आदर्श है।
प्रश्न 5:
‘सत्य की जीत के आधार पर दुःशासन का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ के एक प्रमुख पुरुष पात्र (दुःशासन) के चरित्र की विशेषताएँ बताइट।
या
‘सत्य की जीत’ में व्यक्त दुःशासन के चरित्र की समीक्षा कीजिए।
उत्तर:
प्रस्तुत खण्डकाव्य में दुःशासन एक प्रमुख पात्र है जो दुर्योधन का छोटा भाई तथा धृतराष्ट्र का पुत्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं-
(1) अहंकारी एवं बुद्धिहीन – दुःशासन को अपने बल पर बहुत अधिक घमण्ड है। विवेक से उसे कुछ लेना-देना नहीं है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण मानता है तथा पाण्डवों का भरी सभा में अपमान करता है। सत्य, प्रेम और अहिंसा की अपेक्षा वह पाशविक शक्तियों को ही सब कुछ मानता है
शस्त्र जो कहे वही है सत्य, शस्त्र जो करे वही है कर्म ।
शस्त्र जो लिखे वही है शास्त्र, शस्त्र-बल पर आधारित धर्म ॥
इसीलिए परिवारजन और सभासदों के बीच द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में वह तनिक भी लज्जा नहीं मानता है।
(2) नारी का अपमान करने वाला – द्रौपदी के साथ हुए तर्क-वितर्क में दु:शासन का नारी के प्रति पुरातन और रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। दु:शासन नारी को पुरुष की दासी और भोग्या तथा पुरुष से दुर्बल मानता है। नारी की दुर्बलता का उपहास उड़ाते हुए वह कहता है
कहाँ नारी ने, ले तलवार, किया है पुरुषों से संग्राम ।
जानती है वह केवल पुरुष, भुजदण्डों में करना विश्राम ॥
(3) शस्त्र-बल विश्वासी – दु:शासन शस्त्र-बल को सब कुछ समझता है। उसे धर्म-शास्त्र और धर्मज्ञों में कोई विश्वास नहीं है। इन्हें तो वहें शस्त्र के आगे हारने वाले मानता है ।
धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षणभर चिन्ता इसकी न।
शास्त्र की चर्चा होती वहाँ, जहाँ नर होता शस्त्र-विहीन ।।
(4) दुराचारी – दु:शासन हमारे समक्ष एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में आती है। वह मानवोचित व्यवहार भी नहीं जानता। वह अपने बड़ों व गुरुजनों के सामने भी अभद्र व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। वह शास्त्रज्ञों, धर्मज्ञों व नीतिज्ञों पर कटाक्ष करता है और उन्हें दुर्बल बताता है
लिया दुर्बल मानव ने ढूँढ, आत्मरक्षा का सरल उपाय।
किन्तु जब होता सम्मुख शस्त्र, शास्त्र हो जाता निरुपाय ॥
(5) धर्म और सत्य का विरोधी – धर्म और सत्य का शत्रु दु:शासन आध्यात्मिक शक्ति का विरोधी एवं भौतिक शक्ति का पुजारी है। वह सत्य, धर्म, न्याय, अहिंसा जैसे उदार आदर्शों की उपेक्षा करता है।
(6) सत्य व सतीत्व से पराजित – दुःशासन की चीर-हरण में असमर्थता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सत्य की ही जीत होती है। वह शक्ति से मदान्ध होकर तथा सत्य, धर्म एवं न्याय की दुहाई देने को दुर्बलता का चिह्न बताता हुआ जैसे ही द्रौपदी का चीर खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही द्रौपदी के शरीर से प्रकट होने वाले सतीत्व की ज्वाला से पराजित हो जाता है।
दुःशासन के चरित्र की दुर्बलताओं या विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए डॉ० ओंकार प्रसाद माहेश्वरी लिखते हैं कि “लोकतन्त्रीय चेतना के जागरण के इस युग में अब भी कुछ ऐसे साम्राज्यवादी प्रकृति के दुःशासन हैं, जो दूसरों के बढ़ते मान-सम्मान को नहीं देख सकते तथा दूसरों की भूमि और सम्पत्ति को हड़पने के लिए प्रतिक्षण घात लगाये हुए बैठे रहते हैं। इस काव्य में दुःशासन उन्हीं का प्रतीक है।”
प्रश्न 6:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र-चित्रण कीजिए।
उत्तर:
श्री द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी कृत ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में दुर्योधन एक प्रमुख पुरुष पात्र है जो दु:शासन का बड़ा भाई तथा धृतराष्ट्र का पुत्र है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
(1) अभिमानी और विवेकहीन – दुर्योधन को अपने बाहुबल पर अत्यधिक घमण्ड है। विवेक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह बाहुबल में विश्वास रखता है। नैतिकता में उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण मानता है, इसी कारण पाण्डवों का भरी सभा में अपमान करता है। दुर्योधन का नारी के प्रति पुरातन रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। वह पाशविक शक्तियों को ही सब कुछ मानता है।
(2) नारी के प्रति उपेक्षा-भाव – द्रौपदी के द्वारा उपहास किये जाने पर वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना में दग्ध रहता है। वह नारी को भोग्या और चरणों की धूल समझता है। इसी कारण भरी सभा में द्रौपदी का चीर-हरण करवाता है।
(3) दुराचारी – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में दुर्योधन हमारे सामने एक दुराचारी पुरुष पात्र के रूप में आता है। वह मानवोचित व्यवहार भी नहीं जानता है। वह अपने बड़ों व गुरुजनों के सामने भी अभद्र व्यवहार करने में संकोच नहीं करता।
(4) ईष्र्यालु – दुर्योधन ईष्र्यालु प्रवृत्ति का पुरुष पात्र है, जो हमेशा ही पाण्डवों से ईर्ष्या रखता है। वह पाण्डवों की समृद्धि और मान सम्मान को सहन नहीं कर सकता है।
(5) छल-कपट में विश्वास – दुर्योधन यद्यपि वीर है लेकिन वह छल-कपट में विश्वास रखता है। छल-कपट से ही वह पाण्डवों को जुए के खेल में हरा देता है और उनके राज्य को हड़प लेता है। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके चरित्र में वर्तमान साम्राज्यवादी शासकों की लोलुपता की झलक प्रस्तुत की गयी है।
प्रश्न 7:
‘सत्य की जीत के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र-चित्रण कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए।
उत्तर:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में युधिष्ठिर का चरित्र धृतराष्ट्र और द्रौपदी के कथनों के माध्यम से उजागर हुआ है। उनकी चारित्रिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) सत्य और धर्म के अवतार – युधिष्ठिर की सत्य और धर्म में अडिग निष्ठा है। उनके इसी गुण पर मुग्ध धृतराष्ट्र कहते हैं
युधिष्ठिर ! धर्मपरायण श्रेष्ठ, करो अब निर्भय होकर राज्य।
(2) सरल-हृदय व्यक्ति – युधिष्ठिर बहतं सरल-हृदय के व्यक्ति हैं। वे दसरों को भी सरल-हृदय समझते हैं। इसी सरलता के कारण वे शकुनि और दुर्योधन के कपटे जाल में फंस जाते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। द्रौपदी ठीक ही कहती है
युधिष्ठिर ! धर्मराज थे, सरल हृदय, समझे न कपट की चाल।
(3) सिन्धु-से धीर-गम्भीर – द्रौपदी का अपमान किये जाने पर भी युधिष्ठिर का मौन व शान्त रहने का कारण उनकी दुर्बलता नहीं, वरन् उनकी धीरता, गम्भीरता और सहिष्णुता है
खिंची है मर्यादा की रेखा, वंश के हैं वे उच्च कुलीन।।
(4) अदूरदर्शी – युधिष्ठिर यद्यपि गुणवान हैं, किन्तु द्रौपदी को दाँव पर लगाने जैसा अविवेकी कार्य कर बैठते हैं, जिससे जान पड़ता है कि वह सैद्धान्तिक अधिक किन्तु व्यवहारकुशल कम हैं। वह इस कृत्य का दूरगामी परिणाम दृष्टि से ओझल कर बैठते हैं
युधिष्ठिर धर्मराज का हृदय, सरल-निर्मल-निश्छल-निर्दोष।
भेरा अन्तर-सागर में अमित, भाव-रत्नों का सुन्दर कोष ॥
(5) विश्व-कल्याण के साधक – युधिष्ठिर का लक्ष्य विश्व-मंगल है, यह बात धृतराष्ट्र भी स्वीकार करते हैं
तुम्हारे साथ विश्व है, क्योंकि, तुम्हारा ध्येय विश्व-कल्याण।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खण्डकाव्य के ऐसे पात्र हैं, जो आरम्भ से लेकर अन्त तक मौन रहे हैं। कवि ने उनके मौन से ही उनके चरित्र की उपर्युक्त विशेषताएँ स्पष्ट की हैं।
प्रश्न 8:
‘सत्य की जीत’ की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
या
‘सत्य की जीत’ की भाषा-शैली की विशेषताएँ बताइए।
या
काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से ‘सत्य की जीत का मूल्यांकन कीजिए।
या
एक खण्डकाव्य के रूप में सत्य की जीत का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर:
‘सत्य की जीत’ की काव्यगत विशेषताएँ निम्नवत् हैं
(अ) भावगत विशेषताएँ
(1) सुगठित कथावस्तु – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु अत्यन्त स्पष्ट, सरल और सुगठित है। काव्य की सभी घटनाएँ परस्पर सुसम्बद्ध हैं। कथा में आदि से अन्त तक रोचकता एवं कौतूहल विद्यमान है। कथा में कहीं भी अस्वाभाविकता एवं अरोचकता नहीं है।
(2) विश्व-बन्धुत्व का सन्देश – कवि ने विश्व को ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में प्रेम, सत्य, न्याय, मैत्री, करुणा और सदाचार की शिक्षा देकर सम्पूर्ण संसार को मार्ग दिखाया है
न्याय समता मैत्री भ्रातृत्व, भावना, स्नेहित सह अस्तित्व।
इन्हीं शाश्वत मूल्यों से बने, विश्व का मंगलमय व्यक्तित्व ॥
(3) शान्ति की कामना – ‘सत्य की जीत’ गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। केवल शस्त्र-बल पर विश्वास रखने वाले दुर्योधन और दु:शासन दोनों सत्य, न्याय और शास्त्र से पराजित होते हैं। स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए धृतराष्ट्र कहते हैं
किये हैं जितने भी एकत्र, शस्त्र तुमने, उनका उपयोग।
युद्ध के हित नहीं, शान्ति हित करो, यही है उनका स्वत्व प्रयोग।
(4) उदात्त आदर्शों का स्वर – प्रस्तुत खण्डकाव्य से नारियों के प्रति श्रद्धा, विनाशकारी आचरण, शस्त्रीकरण का विरोध, प्रजातान्त्रिक आदर्शो, असत्य की निर्बलता एवं सत्य के आत्मबल की शक्ति का स्वर मुखरित होता है। इस खण्डकाव्य में कवि ने द्रौपदी के चीर-हरण को प्रसंग बनाकर उदात्त आदर्शों की. भाव-धारा प्रवाहित की है। यह भाव-धारा ही इस खण्डकाव्य की आत्मा है।
(5) रस-निरूपण – प्रस्तुत खण्डकाव्य में वीर रस की प्रधानता है, किन्तु इसमें रौद्र, शान्त आदि रसों का भी सुन्दर परिपाक हुआ है। ओजस्विनी, वीरांगना, द्रौपदी की ओजमयी वाणी इस काव्य का केन्द्रीय आकर्षण है। रौद्र रस का एक उदाहरण द्रष्टव्य है:
मौन हो जा मैं सह सकती न, कभी भी नारी का अपमान।
दिखा देंगी तुझको अभी, गरजती आँखों का तूफान ।
(6) प्रतीकात्मकता – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में सभी पुरुष तथा स्त्री पात्रों का चरित्र प्रतीकात्मक है। द्रौपदी सत्य, न्याय, धर्म आदि गुणों की प्रतीक और अपने अधिकारों के लिए सजग नारी है। पाण्डवों की प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है
युधिष्ठिर सत्य, भीम है शक्ति, कर्म के अर्जुन हैं अवतार।
नकुल श्रद्धा, सेवा सहदेव, विश्व के हैं ये मूलाधार ॥
इसके बाद भी पाण्डवों के सभी गुण द्रौपदी की तेजस्विता के सम्मुख हीन जान पड़ते हैं।
(ब) कलागत विशेषताएँ
(1) भाषा – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की भाषा सरल, सुबोध और परिष्कृत खड़ी बोली है। इसकी भाषा में प्रवाहमयता, प्रभावात्मकता, स्वाभाविकता, प्रसंगानुकूलता आदि गुण भी विद्यमान हैं। काव्य में संवादों की सजीवता एवं प्रभावपूर्णता निस्सन्देह सराहनीय है। भाषा में कहीं भी अस्वाभाविकता एवं दुरूहता के दर्शन नहीं होते; यथा
किया यदि शस्त्रों से ही मोह, न अपनाया विवेक का पन्थ।
मुझे लगता है, जो कुछ हुई, प्रगति अब तक, उसका रे अन्त ।।
(2) शैली – सारा खण्डकाव्य संवादात्मक शैली में रचित है। इसकी सम्पूर्ण कथावस्तु धृतराष्ट्र की राजसभा में पात्रों के कथोपकथनों के रूप में प्रस्तुत की गयी है। संवादों पर आधारित कथा की प्रगति शैली की प्रमुख विशेषता है
द्रौपदी बढ़-बढ़कर मत बोल, कहा उसने तत्क्षण तत्काल।
पीट मत री नारी का ढोल, उगल मत व्यर्थ अग्नि की ज्वाल॥
संवादों के कारण इस काव्य में नाटकीय-सौन्दर्य आ गया है। काव्य के समस्त घटना-व्यापार को सजीव, प्रवाहपूर्ण, सरल और विचारोत्तेजक संवादों के माध्यम से दृश्यांकित किया गया है। इन संवादों में कवि की अपूर्व मनोवैज्ञानिकता एवं सूझ-बूझ का परिचय मिलता है।
(3) अलंकार-योजना – ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है; यथा
रूपक – खोल जीवन-पुस्तक के पृष्ठ, मुस्कराते समरांगण बीच।
शस्त्र से लिखते सच्चे शास्त्र, रक्त के स्वर्णिम अक्षर खींच।
उपमा – माँग में सिन्दूर की यह रेख, मौन विद्युत-सी घन के बीच।
कि जैसे अवसर पाकर शीघ्र, गिराएगी दुश्मन पर खींच ॥
(4) छन्द-विधान – ‘सत्य की जीत में कवि ने 16-16 मात्राओं के चार पंक्तियों वाले; मुक्त छन्द का प्रयोग किया है।
(5) भाव-चित्रण – मानव-हृदय में किसी भाव के उठने पर कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। इन्हें अनुभाव या संचारी भाव कहते हैं। ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि ने विभिन्न-पात्रों के अनुभावों का चित्रण किया है। यहाँ क्रोधाभिभूत भीम की मुद्राओं का चित्रण देखिए
फड़कने लगे भीम के अंग, शस्त्र-बल की सुनकर ललकार।
नेत्र मुड़े धर्मराज की ओर, झुके पी, मौन रक्त की धार ।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि उदात्त आदर्शों के लिए सद्गुणी नायिका को आधार बनाकर लिखी गयी यह काव्य-रचना कथा की लघुती, क्रम-विस्तार आदि गुणों से युक्त है, अत: काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से ‘सत्य की जीत’ एक सफल खण्डकाव्य है।
प्रश्न 9:
” ‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में आज की आधुनिक जाग्रत नारी का स्वर मुखर हुआ है।” इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में द्रौपदी द्वारा प्रतिपादित नारी की शक्ति एवं महत्ता पर प्रकाश डालिटी:
या
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य के आधार पर द्रौपदी और दुःशासन के वार्तालाप (संवाद) को अपने शब्दों में लिखिए।
या
” ‘सत्य की जीत’ में महाभारत युग के साथ वर्तमान युग भी बोल उठा है। इस कथन को समझाइट।
या
‘सत्य की जीत’ कथनक की वर्तमान सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
या
नारी जागरण की दृष्टि से सत्य की जीत’ खण्डकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
‘सत्य की जीत’ खण्डकाव्य में कवि द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी ने द्रौपदी के परम्परागत चरित्र में नवीन उद्भावनाएँ करके आज की नारी का मार्गदर्शन किया है। दूसरे शब्दों में, हम यह भी कह सकते हैं कि माहेश्वरी जी ने द्रौपदी के माध्यम से आधुनिक नारी के उभरते स्वर को सशक्त अभिव्यक्ति दी है, जिसका विवेचन निम्नवत् है
दुःशासन द्वारा भरी-सभा में अपमानित हुई द्रौपदी अबला-सी बनकर केवल आँसू नहीं बहाती, वरन् वह साहसी आधुनिक स्त्री की भाँति सिंहनी के समान गरजती हुई क्रोधित होकर उसे चेतावनी देती है
अरे-ओ ! दुःशासन निर्लज्ज ! देख तू नारी का भी क्रोध।
किसे कहते उसका अपमान, कराऊँगी मैं इसका बोध ॥
द्रौपदी दु:शासन को अपमानित करती हुई बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि तू मुझे बाल खींचकर भरी-सभा में ले तो अवश्य आया है, किन्तु मैं रक्त के बूंट पीकर केवल इसलिए चुप हूँ; क्योंकि नारी से मार खाकर तू संसार में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाएगा।
द्रौपदी के व्यंग्य बाणों से दु:शासन तिलमिला उठता है और कहता है कि “तू नारी की श्रेष्ठता के ढोल मत पीट। क्या कभी किसी नारी ने तलवार अपने हाथ में लेकर कहीं संग्राम किया है ? नारी तो पुरुष पर निर्भर रहती है। वह तो पुरुष के पैरों की धूल के समान है।”
इस पर द्रौपदी नारी-विषयक पुरातन मान्यताओं को तोड़ती हुई दु:शासन को फटकारती हुई कहती है कि “तू अभी नारी की शक्ति को पहचान ही नहीं पाया है। यद्यपि नारी दिखने में कोमल-कलिका के समान अवश्य होती है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह पापियों का संहार करने के लिए भैरवी का रूप भी धारण कर सकती है। पुरुष की यह भूल ही है कि वह सारे विश्व पर अपना अधिकार मानता है, नारी पर अकारण ही चोट करता है, जबकि नारी और पुरुष दोनों एक समान हैं।”
द्रौपदी के व्यंग्य-कटाक्षों को काटते हुए दु:शासन पुनः कहता है कि “नारीरूपी सरिताएँ क्या कभी पुरुषरूपी पहाड़ को हिला पायी हैं ? लहरों को तो भूधर के केवल चरण छूकर लौट जाना पड़ता है। स्त्रीरूपी लहर तो पुरुषरूपी किनारा पाकर शान्त हो जाती है।’ दुःशासन पुनः कहता है कि “तू हमारी दासी है, क्योंकि पाण्डव तुझे जुए में हार गये हैं। तू नारीत्व की बात मत कर।”
इस प्रकार द्रौपदी और दु:शासन के वार्तालाप द्वारा कवि ने यह सिद्ध किया है कि मानवता के विकास में नारी और पुरुष दोनों का ही समान महत्त्व है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ‘पुरुष का स्थान उच्च और नारी का स्थान निम्न है’ ऐसा सोचना नारी के प्रति अन्याय व असत्य का द्योतक है। इस रूप में, ‘सत्य की जीत’ में स्थल-स्थल पर आज की जाग्रत नारी का स्वर ही मुखरित हुआ प्रतीत होता है। ऐसी जाग्रत नारी, जो अपनी सृजनात्मक महत्ता से भली-भाँति परिचित है और जो समय आने पर सीता ही नहीं चण्डी तथा काली भी बन सकती है
पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण।
अन्तत: द्रौपदी और दु:शासन के वार्तालाप का अन्त ‘सत्य की जीत’ से होता है।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी) , drop a comment below and we will get back to you at the earliest.