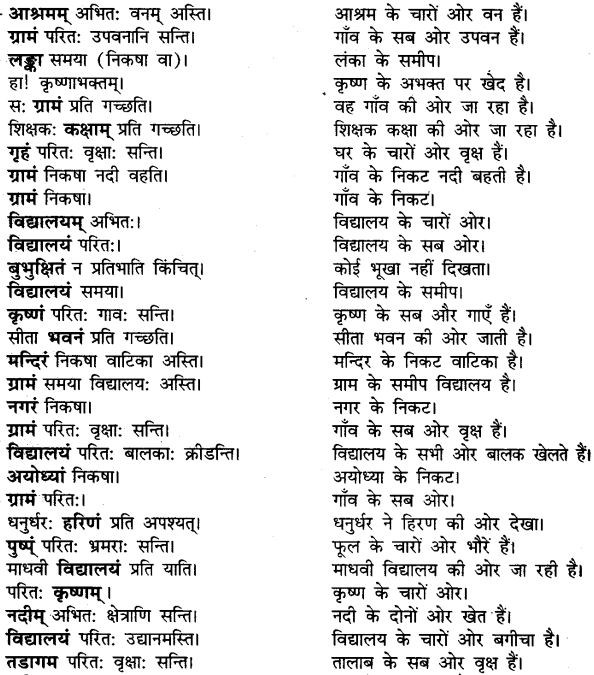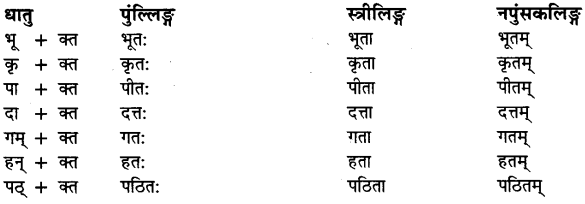UP Board Solutions for Class 12 English Translation Chapter 2 Tenses (Active Voice and Passive Voice) are part of UP Board Solutions for Class 12 English. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 English Translation Chapter 2 Tenses (Active Voice and Passive Voice).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | English Translation |
| Chapter Name | Tenses |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 English Translation Chapter 2 Tenses
Exercise 1
- Pramod worships God every morning.
- He never abuses anyone.
- What do you do at noon ?
- Does your father live in Delhi ?
- I keep my books clean.
- The teacher gives us test every weak.
- My mother loves me.
- Why does your sweeper not come daily?
- Who sings song in this room?
- Why does the judge not listen to the case carefully ?
- The peon rings the second bell at quarter to ten.
- How many times do you have tea in a day?
- Our father always speaks the truth.
- How many languages do you know ?
- Do you go to Delhi by train daily?
Exercise 2
- He is teaching us geography.
- I am not telling you a story.
- Why are you wasting your time?
- Is the sun setting in the west ?
- Are the students sitting in the class ?
- How many gardeners are working in this garden ?
- I will celebrate my birthday the day after tomorrow.
- The hunter is not killing the lion.
- This boy is not telling a lie.
- Where is the police searching for the criminals ?
- Are you reading in the moonlight ?
- Where is your dog sleeping ?
- Who is standing on the roof?
- I am not talking to you.
- She is teaching French in Kolkata university.
Exercise 3
- He has washed his clothes.
- I have not had my food yet.
- Has he left this school forever?
- Why have you not bathed ?
- The peon has not opened the rooms yet.
- The clock has not struck twelve yet.
- The sun has risen in the east.
- Why have you .. not marked this boy present ?
- Have you learnt this question by heart ?
- The judge has given judgement in favour of the teachers.
- The teachers have called off the strike in the interest of the students.
- Why has the government not fullfilled the promise to the teachers ?
- Have you decided to resign from the post ?
- How many people has the police arrested ?
- Has the washerman ironed all the clothes ?
Exercise 4
- Where have you been walking for two hours ?
- The hunters have been chasing the lion since morning.
- The barber has been shaving this man for ten minutes.
- I have not been writing for one year.
- Why has your horse not been eating grass for two days ?
- The child has been weeping for one hour.
- How many boys have been playing cricket match since yesterday ?
- I have been teaching in this school for twenty years.
- We have been fighting elections since 1976.
- Our opponent has been defeating us since then.
- These girls have been knitting sweater since midnight.
- Where has father been reading newspaper for ten minutes ?
- Why have you not been going for a walk since Sunday?
- Has your sister been learning to sing song for one month ?
- The gardener has been watering plants since 4 o’ clock.
Exercise 5
The sun always rises in the east and sets in the west. But the stars twinkle all around the sky at night. At this time it is getting dark because the sun has set in the west. I have been playing in the play ground since 5 o’clock. But now there is no player in the field. All have gone home respectively. Only two of my friends are standing in the wait of mine. I too am going back home. Do you also play some game daily, At what time do you reach the playground? Now our examinations are at hand. But I have made my preparations for the examination in full. I have been working hard for two months. This year our examinations are going to begin on 25th Feb. Have you also completed preparations for the examination in full. In which class does your elder sister study? I got up at 5 in morning and walk about in the park for half an hour. Do you also go for a walk in morning? Where do you walk about? Walking in morning is good for health.
Exercise 6
- Sunil Dutt reached Amritsar yesterday.
- I could not return your book yesterday.
- Did India buy arms from America ?
- Why did you not take part in the match ?
- He talked to his sons at the time of death.
- Our uncle never smoked.
- Why did these boys make their clothes dirty ?
- Our washer man did not bring our clothes yesterday.
- Who issued books to the students in the library ?
- The doctor could not give me good medicine.
- My brother made a lengthy speech.
- Why could you not go to Delhi yesterday ?
- Did you see the picture with your friends ?
- These children never drank cow milk.
- Ram taught English to my two children.
Exercise 7
- 1. The water carriers were sprinkling water on the roads.
- 2. The garlands of flowers were hanging on the doors.
- 3. No sick man was roaming on the roads:
- 4. Was the sunlight making the city beautiful ?
- 5. Who was welcoming the prince ?
- A sick man was crying for help.
- They were not thinking anything about the future.
- Was Siddhartha looking at the old man attentively ?
- When was your friend deceiving you?
- The poets were singing their poems.
- Which word we e you searching for in the dictionary?
- Our father was not going on pilgrimage last year.
- Why were you not obeying your father ?
- Our teacher was not teaching us this lesson yesterday.
- How much milk were you buying yesterday ?
Exercise 8
- He had done this work before he went to Kolkata.
- Had you not departed before you received my letter ?
- Did he have food after you had reached ?
- The birds had flown from the tree even before the sun had risen.
- Did the thief run away after the police had come ?
- He did not stop working hard till he had not passed.
- The crowd dispersed after the policeman had fired.
- He had already given this examination.
- I could not reach home after the guests had gone.
- Had his father died before he was born ?
- Why had the audience gone before the speech was over ?
- The circus show had been over before 9 o’clock.
- Where did the students go after it had stopped raining ?
- The train had departed even before he had bought the tickets.
- He wandered till he had not got service.
Exercise 9
- For how many years had you been reading in this school ?
- I had been waiting for you for an hour.
- Had you been taking Inter examination for few years ?
- The birds had not been flying in the air since today morning.
- Had you been living in this house since June ?
- The teachers had not been coming to school for ten days.
- My father had not been smoking for two months.
- Had you been serving in this hotel for a long time?
- How many students had been living in this hostel since last year?
- Whom had you been teaching English since 10 o’clock ?
- This businessman had not been depositing sales tax for five years.
- Where had the watchman been sleeping since 2 o’clock?
- She had been looking after her husband since the time of marriage.
- The watercarrier had not been sprinkling water on the road for one month.
- Whom had you been writing letter to since 7 o’clock ?
Exercise 10
One day wind was blowing too strong in evening and the sun was setting in the west. Some friends went on foot to yisit to the forest. They were six in number. They saw a flower garden at a little distance. Two of the friends were fond of flowers. Leaving their friends they ran into the garden. Two gardeners had reached the garden before they reached. One of the gardeners had been watering the plants for half an hour and the other gardener was looking after the plants. While moving about those boys reached the gardeners. One of the boys told a gardener that they wanted to pluck some flowers but on seeing them they did not pluck the flowers. The gardener asked them if they had not infact, plucked the flowers. One of the friends could not tell a lie. He took out two rose flowers from his pocket and told the gardener that those were the only two flowers that he had plucked. In the meantime the supervisor of the gardener happened to reach there and fine him fifty rupees. The boy grew sad on hearing about the penalty of fifty rupees for speaking the truth. The supervisor explained to him that the punishment is for breaking the rule and is equal to all. The boy got satisfied and begged pardon of the supervisor.
Exercise 11
- I shall meet you in Gandhi Park in the evening.
- We shall not go for a walk today.
- You will leave this school.
- Where will you get admission now?
- I shall never tell a lie.
- Why will mother not make sweets ?
- Will you understand English newspaper ?
- You will have to come here tomorrow.
- Sunil Dutt will give message of peace to the people.
- These boys shall work hard.
- How many boys will go to see Nauchandi today?
- She will never help her mother.
- When will the peon ring the bell ?
- The principal shall pardon your fine.
- How much milk will you have today?
Exercise 12
- The people will be rejoicing on the occasion of Diwali.
- The police will be patrolling the city.
- My friend will not be waiting for me on the station.
- Will your servant not be taking salary ?
- Will that patient be sleeping in bed ?
- Who will be clamouring before me?
- Will the teacher be checking our essay?
- Where will your mother be sleeping ?
- The train will not be arriving in time.
- Where will they be playing the match?
- We shall not be going to Delhi.
- Why will the children be weeping ?
- How many monkeys will be running on the roof?
- How much milk will you be having ?
- When will the teacher be calling me ?
Exercise 13
- They will have gone from here five years ago.
- I will have read the newspaper before father goes out.
- Will he not have returned from picnic tomorrow ?
- This patient will have died before his sons come.
- Will the guests have gone before the sun rises ?
- How many spectators will have seen cricket match by 10th May ?
- I shall not have reached my school by 8 O’clock.
- Who will have knocked at the door before I come out ?
- Will you have drawn the map before the teacher comes ?
- Will the police have arrested the thieves before they run away?
- Why will the carpenter not have prepared all furniture before marriage ?
- Will your examination have been over before 8th April ?
- The enemy will not have run away when our army reaches.
- The cat will have drunk all milk before the mistress awakes.
- All the people will have run away before the storm approaches.
Exercise 14
- Will you have been playing for two hours ?
- He will have been waiting for you for two days.
- What will this boy have been doing here since Friday?
- Will the hunter have been chasing the rabbit for two hours ?
- She will not have been singing song since 3 o’clock.
- Will you have been cleaning your house for two hours ?
- These students will not have been studying English from next year.
- These children will not have been watching T.V. since 7 o’clock
- Where will the police have been chasing the thief for two hours ?
- Where will you have been going to examine the answer books since 15th April ?
- Will your son have been preparing for entrance examination next year?
- The government will not have been giving any relaxation in the taxes from the end of this year.
- Will you have been teaching Hindi also since 2004 ?
- The washer man will have been ironing the clothes for one hour.
- Will you have been reading the newspaper since ten minutes ?
Exercise 15
Where will you celebrate your birthday and how many friends will you invite this year? Will some relatives too participate your birthday function? At least I will be overjoyed in your birthday function as ever. I will be making preparations for so to attend your birthday function for many days before. This time I will give you a unique birthday gift and this will be a surprising gift. All the persons attending the party will be wonders such on seeing it. Although all the persons will bring gifts but the gift of mine will be unique of all. I am saying this with full confidence. You will be receiving your friends at the entrance. All of your friends will be greatly happy to see you in your new dress. Your friends will have been waiting for this day for so many days. Will you also help me in my birthday party. How many hours earlier will you come on my birthday. I will have been waiting for your arrival. You will be all in all in my birthday function. I am confident of it that you will make my birthday function uniqne.
Exercise 16
- The thieves were arrested by the police.
- He was requested for help.
- My friend was shot dead.
- You will not be pardoned.
- The students are fined by the principal,
- The children are looked after by the parents.
- Now these books will be sold.
- A film will be shown to us.
- Will a letter be sent to me?
- Is this boy praised by all the teachers ?
- Was this lesson not taught to the students ?
- When were you abused by him ?
- The patients are given cow milk.
- The story was not told by our grandmother.
- Will you be given the invitation of feast ?
Exercise 17
- This novel is being read by me.
- A message was being sent by them.
- Was a letter being written by the father ?
- A song is being sung by the girls.
- Was a match being played by the boys ?
- The boys are being punished.
- The stones were being thrown on the frogs by the boys.
- Are they being called ?
- By whom are you being taught English ?
- Prizes are being distributed to the boys.
- The car was being driven by the driver.
- Football was being played by the boys.
- Medicine was being given to the patient by the doctor.
- All patients are being vaccinated.
- Rice are being boiled by the mother.
Exercise 18
- The match will have been finished.
- The medicine will have been given to the patient.
- Our work has been finished.
- All the clothes have been washed.
- The lesson has been learnt by the boys.
- The city had been burnt by the enemy.
- The clothes will have been ironed by the washe rman.
- When had the dacoit been hanged ?
- Why have sweets been distributed ?
- The servant will have been given the order.
- The crops had been reaped last month.
- The lessons will have been revised by the students.
- All the plants have been destroyed by the monkeys.
- Two children have been run over by a truck.
- A letter had been written to our friend by us.
Exercise 19
- The answer to this letter must be sent.
- This patient should be admitted in a good nursing home.
- This time the match can be won.
- The cake may be eaten by ants.
- The car should be driven slowly.
- The parents should be obeyed.
- T.V. should be watched from a distance.
- Can this case be heard ?
- The plays of Shakespeare can be enjoyed.
- Medicine must be taken regularly at a proper time.
Exercise 20
- The dogs of this locality are being caught.
- Prizes are being distributed in this school every year.
- The application will be sent to the principal.
- Can all the students be called for practical examination ?
- All your work must be finished before time.
- The animals should not be killed.
- All the prisoners have been released.
- Was this lesson not taught to you yesterday?
- All these patients will be given medicine.
- The invitation of the feast was sent to you.
- The whole city is being decorated to welcome the primeminister.
- How many lessons had been taught before the start of the examination ?
- You will be welcomed with great pomp and show.
- The servant will have been sent home before it is evening.
- Your cow has been milked.
Exercise 21
- She is going to leave Kanpur tomorrow at 12.
- I am going to reach Delhi tomorrow at 6 p.m.
- The prime minister is going to America next week.
- The chief minister is going to take oath tomorrow at 3 pm.
- The parliament session is going to start on 10th February.
- My father comes back to India in August.
- The prime minister is hoisting national flag at 8 o’clock on 15th August.
- The new film of Amitabh Bachchan is going to be released in November.
- I am going to celebrate my 20th birthday this month.
- We go to Shimla on 7th April by the night train.
Exercise 22
- I hear him speaking.
- I hear some women weeping
- I have been waiting for your arrival for a long time.
- I was thinking that I should build a new house.
- This curtain looks bright coloured.
- This scent smells pleasant.
- The paper seems smooth.
- Do you understand what he is saying ?
- This teacher seems polite.
- Your friend seems knave.
- Those grapes taste sour.
- Do you hear the bird sing ?
- Why do you look sad today?
- I smell something burning in the kitchen.
- This shirt looks coarse for summer.
Exercise 23
- Mahadevi Verma has written many poems.
- I read your letter in the morning.
- Munesh died in an accident.
- The doctor has examined your son just now.
- He met me recently.
- He examined all the answer books last evening.
- He met me some time before.
- I have had my lunch at 1 p.m. Now I shall have dinner.
- I studied in this school for two years.
- I have studied in this school for two years.
- I am hearing some people singing.
- I am feeling pleasant smell from your clothes.
- My father lived in America for ten years.
- Have you taken your dinner?
- He is feeling good now.
Exercise 24
- 1. He is clever in telling lies.
- 2. After reading novel he went to the market.
- 3. Sleeping is also necessary for man.
- 4. Swimming is taught in our school.
- 5. He is tired of working.
- 6. Your son will be stopped from watching the film.
- 7. He is fond of playing hockey.
- 8. Sleeping in the daytime is harmful.
- He is very fond of having tea.
- Boasting of one self is bad.
- The Sikhs hate smoking.
- Asking question is easier than solving it.
- Lata’s singing pleased all.
- Your habit of wasting time is not good.
- It is of no use weeping now.
Exercise 25
- Some people worship the rising sun.
- I saw trees loaded with fruits.
- Having retired he started his business.
- A rolling stone gathers no moss.
- Entering the room I found the grandfather dead.
- A hungry fox saw some bunches of grapes hanging from a vine.
- Hearing the noise all the neighbors awoke.
- Turning to the right you will reach the temple.
- I heard her crying bitterly.
- You cannot forget a well learnt lesson.
- Tired players sat down to rest.
- You should have a balanced diet.
- Having finished their work all the clerks went to their homes.
- Having thanked the people the leader finished his speech.
- Having buried the dead body all the people went to their homes.
Exercise 26
- I shall get my house built in Vasundhra.
- Did you get your hair trimmed ?
- She gets tea prepared by her husband.
- By whom do you get your clothes ironed ?
- I have my car washed by the driver.
- Why do you have your floor swept by your son ?
- I did not get my watch mended.
- I shall have my homework done by my elder sister.
- I myself mop the floor.
- I shall have the cobwebs of my room cleaned by him.
Exercise 27
- Why will he have the scrap dealer called ?
- I shall make her cook tasty food.
- He is making Panditji worship.
- Mother is making her elder daughter knit the sweater.
- The passengers were making the driver drive the bus fast.
- The director was making the artist run fast.
- The magician was making the spectators wonder.
- Why does he make me sad ?
- I shall get you scolded by my father.
- Where did the captain make the soldiers run ?
Exercise 28
- I worked hard so that I might pass.
- The landlord found that the thieves had run away with his costly goods.
- An old man told his sons that unity is strength.
- He loved Sonia more than his daughters.
- All people know that the dogs bark at night.
- I met that player who plays badminton well.
- Your brother failed because he was very weak in mathematics.
- Yesterday I met a gentleman who deals in shoes.
- I went to the city where he lives now.
- He cries as if he is hurt.
- There flowed a river where there are fields now.
- Ram loved me more than he loves his brother.
- My class teacher told the principal that I always speak the truth.
- The passengers said that they would not pay more than actual fare.
- My mother will say that I should work hard.
We hope the UP Board Solutions for Class 12 English Translation Chapter 2 Tenses (Active Voice and Passive Voice) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 English Translation Chapter 2 Tenses (Active Voice and Passive Voice), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.