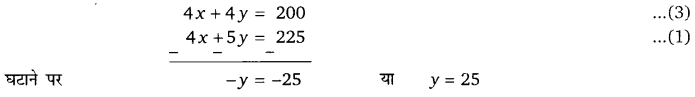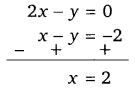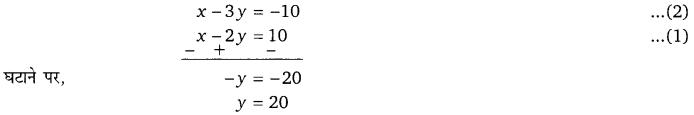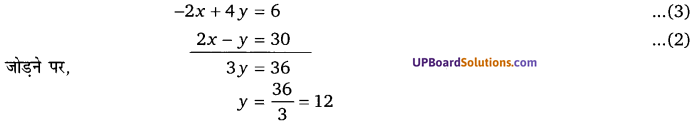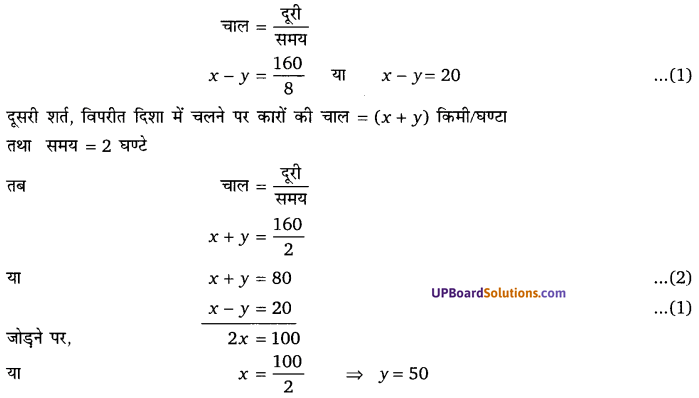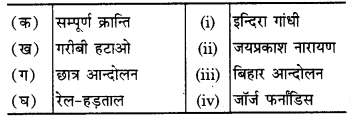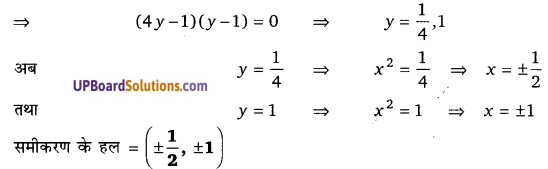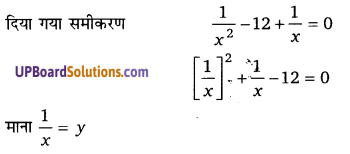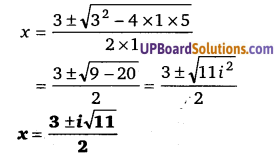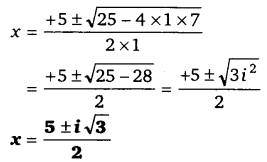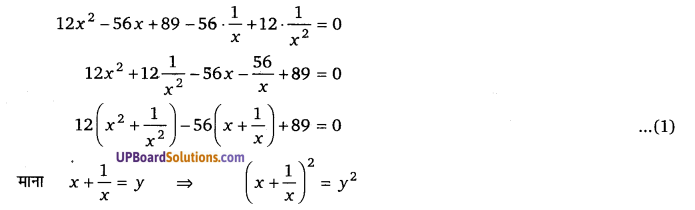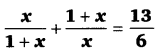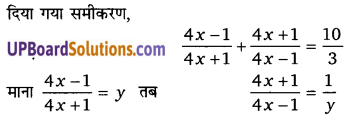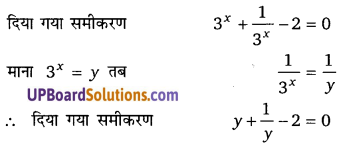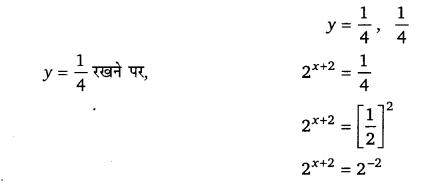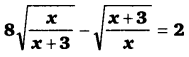UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 8 Environment and Natural Resources
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 Text Book Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1.
पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें-
(क) विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिन्तित हैं।
(ख) पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है।
(ग) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुँच गया है।
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर:
(ग) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुँच गया है।
प्रश्न 2.
निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिह्न लगाएँ। ये कथन पृथ्वीसम्मेलन के बारे में हैं
(क) इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भाग लिया।
(ख) यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में हुआ।
(ग) वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया।
(घ) यह महासम्मेलनी बैठक थी।
उत्तर:
(क) इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भाग लिया।
(ख) यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में हुआ।
(ग) वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया।
(घ) यह महासम्मेलनी बैठक थी।
प्रश्न 3.
‘विश्व की साझी विरासत’ के बारे में निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं-
(क) धरती का वायुमण्डल, अण्टार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अन्तरिक्ष को ‘विश्व की साझी विरासत’ माना जाता है।
(ख) ‘विश्व की साझी विरासत’ किसी राज्य के सम्प्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते।
(ग) ‘विश्व की साझी विरासत’ के प्रबन्धन के सवाल पर उत्तरी व दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है।
(घ) उत्तरी गोलार्द्ध के देश ‘विश्व की साझी विरासत’ को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिन्तित हैं।
उत्तर:
(क) धरती का वायुमण्डल, अण्टार्कटिका, समुद्री सतह व बाहरी अन्तरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। (सही)
(ख) ‘विश्व की साझी विरासत’ किसी राज्य के सम्प्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती। (सही)
(ग) ‘विश्व की साझी विरासत’ के प्रबन्धन के सवाल पर उत्तरी व दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। (सही)
(घ) उत्तरी गोलार्द्ध के देश विश्व की साझी विरासत’ को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिन्तित हैं। (गलत)
प्रश्न 4.
रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए?
उत्तर:
रियो सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में सन् 1992 में ब्राजील के शहर रियो-डी-जेनेरियो में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। यह सम्मेलन पर्यावरण व विकास के मुद्दे पर केन्द्रित था। इस सम्मेलन के अग्रलिखित परिणाम हुए-
(1) इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला।
(2) रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी के सम्बन्ध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए।
(3) भविष्य के विकास के लिए ‘एजेण्डा-21’ प्रस्तावित किया गया जिसमें विकास के कुछ तौर-तरीके भी सुझाए गए। इसमें टिकाऊ विकास की धारणा को विकास रणनीति के रूप में समर्थन प्राप्त हुआ।
(4) इस सम्मेलन में पर्यावरण रक्षा के बारे में धनी व गरीब देशों अथवा उत्तरी गोलार्द्ध व दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के दृष्टिकोण में मतभेद उभरकर सामने आए। भारत व चीन तथा ब्राजील जैसे विकासशील देशों का तर्क था कि चूंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विकसित देशों ने अधिक किया है, अत: वे पर्यावरण प्रदूषण के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। अत: उन्हें पर्यावरण रक्षा हेतु अधिक संसाधन व प्रौद्योगिकी आदि उपलब्ध कराना चाहिए। कई धनी देश इस तर्क से सहमत नहीं थे।
(5) अन्तत: रियो सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का लेकिन अलग-अलग भूमिका का सिद्धान्त स्वीकृत किया गया। इस सिद्धान्त का तात्पर्य है कि पर्यावरण के विश्वव्यापी क्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है जिसे देखते हुए विभिन्न राष्ट्रों की पर्यावरण रक्षा के प्रति साझी, किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारी होगी।
संक्षेप में, रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण का प्रश्न विश्व राजनीति में महत्त्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा।

प्रश्न 5.
‘विश्व की साझी विरासत’ का क्या अर्थ है? इसका दोहन व प्रदूषण कैसे होता है?
उत्तर:
साझी विरासत का अर्थ साझी विरासत का अर्थ उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय स्तर पर नदी, कुआँ, चरागाह आदि साझी सम्पदा के उदाहरण हैं।
विश्व स्तर पर कुछ संसाधन तथा क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी एक देश के सम्प्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, इसलिए उनका प्रबन्धन साझे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे विश्व सम्पदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इस साझी विरासत में पृथ्वी का वायुमण्डल, अण्टार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अन्तरिक्ष शामिल हैं।
विश्व की साझी विरासत का दोहन व प्रदूषण साझी विरासत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन व इनके प्रदूषण का क्रम जारी है। उदाहरण के लिए, यद्यपि सन् 1959 के बाद अण्टार्कटिका महाप्रदेश में मानवीय गतिविधियाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही हैं परन्तु इसके बावजूद इस महादेश के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ, जैसे तेल का रिसाव, के कारण अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। भारत ने अनुसन्धान हेतु अण्टार्कटिका प्रदेश में कई वैज्ञानिक दल भेजे हैं तथा वहाँ भारत का गंगोत्री नामक स्थायी अनुसन्धान केन्द्र भी स्थित है।
इसी तरह क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसों के असीमित उत्सर्जन के कारण वायुमण्डल की ओजोन परत का . क्षरण हो रहा है। 1980 के दशक के मध्य में अण्टार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। ओजोन परत के क्षय होने पर सूरज की पराबैंगनी किरणें मनुष्यों तथा फसलों व पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।
तटीय क्षेत्रों में औद्योगिकी व व्यावसायिक गतिविधियों के कारण समुद्री सतह प्रदूषित हो रही है। कई बार तेल समुद्री सतह पर परत के रूप में फैल जाता है, जिससे समुद्री जीवों व वनस्पतियों को नुकसान होता है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण से ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तथा वायुमण्डल व जलीय स्रोत भी प्रभावित होते हैं। इस प्रदूषण से पारिस्थितिकी व जलवायु परिवर्तन पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।
साझी विरासत की सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण समझौते; जैसे-अण्टार्कटिका सन्धि (1959) माण्ट्रियल प्रोटोकॉल (1991) हो चुके हैं। परन्तु पारिस्थितिक सन्तुलन के सम्बन्ध में अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते रहते हैं, जिससे विश्व समुदाय में सहयोग हेतु आम सहमति बनाना कठिन है।
प्रश्न 6.
‘साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों’ से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं?
उत्तर:
विश्व पर्यावरण की रक्षा के सम्बन्ध में ‘साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ सिद्धान्त के प्रतिपादन का तात्पर्य है कि चूंकि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है। यह जिम्मेदारी विकसित व विकासशील देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती। इसके अलावा अभी गरीब देश विकास के पथ पर गुजर रहे हैं, अत: उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार रियो सम्मेलन ने माना कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।
इसी सन्दर्भ में रियो घोषणा-पत्र का कहना है कि “धरती के पारिस्थितिकी तन्त्र की अखण्डता व गुणवत्ता की बहाली सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सभी राष्ट्र विश्व बन्धुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राष्ट्रों की साझी, किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारी होगी।”
साझी जिम्मेदारी तथा अलग-अलग भूमिका के सिद्धान्त को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन व तत्त्वों के प्रयोग का आकलन किया जाए तथा प्रदूषण रोकने के प्रयासों में उसी अनुपात में उस देश की जिम्मेदारी तय की जाए। पुन: चूँकि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा एक साझा वैश्विक मुद्दा है अत: विकसित देशों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर गरीब देशों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
जो देश अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए हैं तथा अभी विकास की प्रक्रिया में पीछे हैं, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीक प्रदान कर पर्यावरण रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे देश ‘टिकाऊ विकास’ (Sustainable Development) की रणनीति को अपनाने हेतु आकर्षित नहीं होंगे। इसी सिद्धान्त के आधार पर जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में क्योटो प्रोटोकॉल, सन् 1997 में चीन तथा भारत जैसे विकासशील देशों को फ्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन की सीमा में छूट दी गई है।
प्रश्न 7.
वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं?
उत्तर:
वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में निम्नलिखित कारणों से विभिन्न देशों में प्राथमिक सरोकार बन गए हैं-
(1) दुनिया में जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वहीं कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जलाशयों की जलराशि में कमी तथा उनका प्रदूषण, चरागाहों की समाप्ति तथा भूमि के अधिक सघन उपयोग से उसकी उर्वरता कम हो रही है तथा खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या के अनुपात से कम हो रहा है।
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट, 2006 के अनुसार जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण दुनिया की एक अरब बीस करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। 30 लाख से ज्यादा बच्चे प्रदूषण के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं।
(3) वनों के कटाव से जैव-विविधता का क्षरण तथा विपरीत जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हो गया है।
(4) फ्लोरोफ्लोरो कार्बन, गैसों के उत्सर्जन से जहाँ वायुमण्डल की ओजोन परत का क्षय हो रहा है, वहीं ग्रीन हाऊस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से कई देशों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है।
(5) समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण के कारण समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। चूंकि विश्व समुदाय को यह आभास हो गया है कि उक्त समस्याएँ वैश्विक हैं तथा इनका समाधान बिना वैश्विक सहयोग के सम्भव नहीं है, अतः पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का भी अंग बन गया है। प्रत्येक राष्ट्र समूह (विकसित व विकासशील) अपने हितों को ध्यान में रखकर पर्यावरण रक्षा का एजेण्डा प्रस्तुत कर रहा है। परिणामस्वरूप, सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशेष रूप से इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण व विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं, यथा-टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जैविक विविधता, मूल देशी जनता के अधिकार व अलग-अलग भूमिका की धारणा पर विस्तार से चर्चा की गई।
उक्त पृष्ठभूमि में पर्यावरण का मुद्दा विभिन्न राष्ट्रों के लिए प्रथम सरोकार के रूप में उभरकर सामने आया।
हए।

प्रश्न 8.
पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह व सहकार की नीति अपनाएँ। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी व दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर:
पृथ्वी व उसके पर्यावरण को बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिक विकास व प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन के कारण गम्भीर खतरा बना हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण की प्रकृति ऐसी है कि इसे किसी देश की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। इसका प्रभाव वैश्विक है। अत: इसके सुधार के प्रयास भी वैश्विक स्तर पर होने चाहिए।
विश्व पर्यावरण सुरक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग की जो बातचीत चल रही है, उसमें उत्तरी गोलार्द्ध के विकसित देशों तथा दक्षिणी गोलार्द्ध के विकासशील देशों के नजरिए में मतभेद देखने में आया है। विकसित देश पर्यावरण क्षरण के वर्तमान स्तर पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए इसके संरक्षण में सभी राष्ट्रों की समान जिम्मेदारी व भूमिका के हिमायती हैं। इसके विपरीत गरीब देशों का तर्क है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित देशों ने पर्यावरण क्षरण किया है तथा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया है, अतः विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की भूमिका गरीब देशों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। दूसरा, विकासशील देशों में अभी पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है अत: पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी इन देशों की कम होनी चाहिए।
सन् 1992 के अन्तर्राष्ट्रीय रियो सम्मेलन में ये मतभेद खुलकर सामने आए। इसीलिए सम्मेलन के प्रस्ताव के बीच का रास्ता अपनाया गया जिसमें कहा गया कि विश्व पर्यावरण की सुरक्षा व गुणवत्ता में सभी विश्व समुदाय की साझी जिम्मेदारी होगी, परन्तु इस संरक्षण में विकसित व विकासशील देशों की भूमिकाएँ अलग-अलग होंगी। अर्थात् विकसित देश संसाधनों व प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व पर्यावरण की सुरक्षा में अधिक योगदान देंगे।
उपर्युक्त मतभेद के बावजूद यह स्पष्ट है कि विश्व पर्यावरण की वैश्विक समस्या के कारण इसकी सुरक्षा हेतु विश्व सहयोग व सहकार की आवश्यकता है तथा विश्व समूहों को इस दिशा में अधिकाधिक सहयोग हेतु तत्पर होना आवश्यक है।
प्रश्न 9.
विभिन्न देशों के सामने सबसे गम्भीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाएँ।
उत्तर:
गत 50 वर्षों में विश्व में हुए आर्थिक व औद्योगिक विकास से स्पष्ट हो जाता है कि विकास की यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। इसके कारण पारिस्थितिकी सन्तुलन इतना अधिक बिगड़ गया है कि वह मानव समुदाय के लिए एक संकट का रूप धारण कर रहा है। वायुमण्डल में हुए प्रदूषण में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ खड़ी हुई हैं। भूमि तथा जलीय संसाधनों का भी प्रदूषण बढ़ा है। वनों की कटाई से जैविक विविधता तथा जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
अत: विश्व समुदाय ने इस बात पर आवश्यकता अनुभव की कि विकास की रणनीति ऐसी हो जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न न हो। एक वैकल्पिक अवधारणा के रूप में सन् 1978 में छपी बर्टलैण्ड रिपोर्ट (अवर कॉमन फ्यूचर) में टिकाऊ विकास (Sustainable Development) का प्रतिपादन किया गया था। रिपोर्ट में चेताया गया था कि औद्योगिक विकास के चालू तौर-तरीके आगे चलकर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से टिकाऊ साबित नहीं होंगे।
सन् 1992 में रियो सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से टिकाऊ विकास की धारणा पर बल दिया गया था। टिकाऊ विकास रणनीति में विकास के ऐसे साधन अपनाए जाते हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त व जीवन्त बने रहें। इसमें विकास को पर्यावरण रक्षा के साथ जोड़ दिया जाता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विकास का लक्ष्य बन जाता है।
उदाहरण के लिए, वर्तमान में हम ऊर्जा की माँग को देखते हुए गैर-रम्परागत स्रोतों; जैसे—पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू-तापीय, बायो-गैस आदि का दोहन कर सकते हैं, जिससे विकास में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 135 के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन भी संरक्षित रहेंगे। इसी तरह नवीन तकनीक व मशीनों के प्रयोग कर ग्रीन हाऊस गैसों व क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। विकास के साथ वनों का संरक्षण, भू-जल संरक्षण, सामाजिक-वानिकी आदि को अपनाकर हम संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्षतः टिकाऊ विकास की धारणा के द्वारा हम पर्यावरण रक्षा व विकास दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 InText Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
जंगल के सवाल पर राजनीति, पानी के सवाल पर राजनीति और वायुमण्डल के मसले पर राजनीति! फिर किस बात में राजनीति नहीं है!
उत्तर:
वर्तमान में विश्व की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, जहाँ प्रत्येक बात में राजनीति होने लगी है। इससे ऐसा लगता है कि अब कोई विषय ऐसा नहीं बचा है जिस पर राजनीति नहीं हो।
प्रश्न 2.
क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अन्तर है?
उत्तर:
पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अन्तर है। धनी देशों की मुख्य चिन्ता ओजोन परत के छेद और वैश्विक ताप वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) को लेकर है जबकि गरीब देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबन्धन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिन्तित हैं।
धनी देश पर्यावरण के मुद्दे पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस रूप में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि निर्धन देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को हानि अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुँची है। यदि धनी देशों ने पर्यावरण को अधिक हानि पहुँचायी है तो उन्हें इस हानि की भरपाई करने की जिम्मेदारी भी अधिक उठानी चाहिए। साथ ही निर्धन देशों पर वे प्रतिबन्ध न लगें जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं।

प्रश्न 3.
क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करें। किन बड़े देशों ने इस पर दस्तखत नहीं किए और क्यों?
उत्तर:
क्योटो प्रोटोकॉल-जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में 1 दिसम्बर से 11 दिसम्बर, 1997 तक हुआ। इस सम्मेलन में 150 देशों ने हिस्सा लिया और जलवायु परिवर्तन को कम करने की वचनबद्धता को रेखांकित किया। इस प्रोटोकॉल में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्जर्सन को कम करने के लिए सुनिश्चित, ठोस और समयबद्ध उपाय करने पर बल दिया गया।
यद्यपि इस बैठक में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद और अधिक बढ़ गए थे तथापि 11 दिसम्बर, 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल (न्यायाचार) को दोनों प्रकार के देशों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
इस प्रोटोकॉल (न्यायाचार) के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-
- इसमें विकसित देशों को अपने सभी छह ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन स्तर को सन् 2008 से 2012 तक सन् 1990 के स्तर से औसतन 5.2% कम करने को कहा गया।
- यूरोपीय संघ को सन् 2012 तक ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन स्तर में 8%, अमेरिका को 7%, जापान तथा कनाडा को 6% की कमी करनी होगी, जबकि रूस को अपना वर्तमान उत्सर्जन स्तर सन् 1990 के स्तर पर बनाए रखना होगा।
- इस अवधि में ऑस्ट्रेलिया को अपने उत्सर्जन स्तर को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने की छूट दी गई।
- विकासशील देशों को निर्धारित लक्ष्य के उत्सर्जन स्तर में कमी करने की अनुमति दी गई।
- इस प्रोटोकॉल में उत्सर्जन के दायित्वों की पूर्ति के लिए विकासशील देश विकास में स्वैच्छिक भागीदारी में शामिल होंगे। इस हेतु विकासशील देशों में पूँजी निवेश करने के लिए विकसित देशों को ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रश्न 4.
लोग कहते हैं कि लातिनी अमेरिका में एक नदी बेच दी गई। साझी सम्पदा कैसे बेची जा सकती है?
उत्तर:
साझी सम्पदा का अर्थ होता है-ऐसी सम्पदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख-रखाव के सन्दर्भ में समूह के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और समान उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। लेकिन वर्तमान में निजीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पारिस्थितिकी तन्त्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी सम्पदा का आकार घट रहा है। गरीबों को साझी सम्पदा की उपलब्धता कम हो रही है। सम्भवत: लातिनी अमेरिका में इन्हीं कारणों से नदी पर किसी मनुष्य समुदाय या राज्य ने अधिकार कर लिया हो और वह साझी सम्पदा न रही हो। ऐसी स्थिति में उसे उसके स्वामित्व वाले समूह ने किसी अन्य को बेच दिया हो। इस प्रकार साझी सम्पदा को निजी सम्पदा में परिवर्तित कर उसे बेचा जा रहा है।
प्रश्न 5.
मैं समझ गया! पहले उन लोगों ने धरती को बर्बाद किया और अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है। क्या यही है हमारा पक्ष?
उत्तर:
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित बुनियादी नियमाचार में चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश (जैसे-ब्राजील, चीन और भारत) नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका कहना है कि भारत पर इस तरह की बाध्यता अनुचित है क्योंकि सन् 2030 तक उसकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर मात्र 1.6 ही होगी, जो आधे से भी कम होगी। बावजूद विश्व के (सन् 2000) औसत (3.8 टन/प्रति व्यक्ति) के आधे से भी कम होगा।
भारत या विकासशील देशों के उक्त तर्कों को देखते हुए यह आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है कि पहले उन लोगों ने अर्थात् विकसित देशों ने धरती को बर्बाद किया, इसलिए उन पर उत्सर्जन कम करने की बाध्यता को लागू करना न्यायसंगत है और विकासशील देशों में कार्बन की दर कम है इसलिए इन देशों पर बाध्यता नहीं लागू की जाए। इसका यह अर्थ निकाला गया है कि अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है।
लेकिन भारत या विकासशील देशों का अपना पक्ष रखने का यह आशय नहीं है बल्कि आशय यह है कि विकासशील देशों में अभी कार्बन उत्सर्जन दर बहुत कम है तथा सन् 2030 तक यह मात्र 1.6 टन/प्रति व्यक्ति ही होगी, इसलिए इन देशों को अभी इस नियमाचार की बाध्यता से छूट दी जाए ताकि वे अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकें। साथ ही ये देश स्वेच्छा से कार्बन की उत्सर्जन दर को कम करने का प्रयास करते रहेंगे।
प्रश्न 6.
क्या आप पर्यावरणविदों के प्रयास से सहमत हैं? पर्यावरणविदों को यहाँ जिस रूप में चित्रित किया गया है क्या आपको वह सही लगता है?
उत्तर:
चित्र में दर से पर्यावरणविदों को अपने किसी उपकरण से वृक्ष को जाँचते हुए या पानी देते हुए दिखाया गया है। एक व्यक्ति के पीछे पाँच प्राणी खड़े हैं। वे वृक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पेड़ पर एक खम्भा है जिस पर विद्युत की तार दिखाई देती हैं। शायद वे पेड़ को सूखा समझकर इसे काटे जाने की सिफारिश करना चाहते हैं। वे विशेषज्ञ होते हुए पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों को नहीं देख रहे हैं। वे पर्यावरण के संरक्षण में स्थानीय लोगों के ज्ञान, अनुभव एवं सहयोग की भी बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अत: यह चित्र पर्यावरणविदों को जिस रूप में चित्रित कर रहा है, वह सही नहीं लगता।
प्रश्न 7.
पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज्यादा और भूमि का विस्तार कम है। फिर भी, कार्टूनिस्ट ने जमीन को पानी की अपेक्षा ज्यादा बड़े हिस्से में दिखाने का फैसला किया है। यह कार्टून किस तरह पानी की कमी को चित्रित करता है?
उत्तर:
पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज्यादा और भूमि का विस्तार कम है। फिर भी, कार्टूनिस्ट ने जमीन को पानी की अपेक्षा ज्यादा बड़े हिस्से में दिखाने का फैसला किया है। यह कार्टून विश्व में पीने योग्य जल की कमी को चित्रित करता है।
विश्व के कुछ भागों में पीने योग्य साफ पानी की कमी हो रही है तथा विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस जीवनदायी संसाधन की कमी के कारण हिंसक संघर्ष हो सकते हैं। कार्टूनिस्ट ने इसी को इंगित करते हुए विश्व में जमीन की तुलना में पानी की मात्रा को कम दिखाया है क्योंकि समुद्रों का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए इसे इस जल मात्रा में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न 8.
आदिवासी जनता और उनके आन्दोलनों के बारे में कुछ ज्यादा बातें क्यों नहीं सुनायी पड़तीं? क्या मीडिया का उनसे कोई मनमुटाव है?
उत्तर:
आदिवासी जनता और उनके आन्दोलनों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लम्बे समय तक उपेक्षित रहे हैं। इसका प्रमुख कारण मीडिया के लोगों तक इनके सम्पर्क का अभाव रहा है। सन् 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के आदिवासियों के नेताओं के बीच सम्पर्क बढ़ा है। इससे उनके साझे अनुभवों और सरकारों को शक्ल मिली है तथा सन् 1975 में इन लोगों की एक वैश्विक संस्था ‘वर्ल्ड काउंसिल
ऑफ इण्डिजिनस पीपल’ का गठन हुआ तथा इनसे सम्बद्ध अन्य स्वयंसेवी संगठनों का गठन हुआ। अब इनके मुद्दों तथा आन्दोलनों की बातें भी मीडिया में उठने लगी हैं। अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी लोगों की संस्थाओं के न होने के कारण मीडिया में इनकी बातें अधिक नहीं सुनाई पड़ती हैं। जैसे-जैसे आदिवासी समुदाय अपने संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करता जाएगा, इन संगठनों के माध्यम से इनके मुद्दे और आन्दोलन भी मीडिया में मुखरित होंगे।
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 Other Important Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 8 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
मूलवासी कौन हैं? मूलवासियों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए।
अथवा मूलवासियों का अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन एवं इनकी प्राप्ति हेतु वैश्विक प्रयासों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मूलवासी से आशय संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर किसी अन्य संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया।
ये मूलवासी आज भी सम्बन्धित देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से अधिक अपनी परम्परा, सांस्कृतिक रीति-रिवाज एवं अपने विशेष सामाजिक-आर्थिक तौर-तरीकों पर जीवन-यापन करना पसन्द करते हैं।
मूलवासियों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष एवं आन्दोलन
भारत सहित वर्तमान विश्व में मूलवासियों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है। दूसरे सामाजिक आन्दोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेण्डा और अधिकारों की आवाज उठाते रहे जिनका विवरण निम्नानुसार हैं-
1. विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आन्दोलन-मूलवासियों को एक लम्बे समय से सभ्य समाज में दोयम दर्जे का माना जाता था। उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। वर्तमान विश्व में शेष जनसमुदाय के अपने प्रति निम्न स्तर के व्यवहार को देखकर इन्होंने विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए अपनी आवाज बुलन्द की है।
2. स्वतन्त्र पहचान की माँग-मूलवासियों के निवास स्थान मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं भारत में हैं, जहाँ इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड सहित ओसियाना क्षेत्र के बहुत-से द्वीपीय देशों में हजारों वर्षों से पॉलिनेशिया, मैलनेशिया एवं माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी निवासरत् हैं। इन मूलवासियों की अपने देश की सरकारों से माँग है कि इन्हें मूलवासी के रूप में अपनी स्वतन्त्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए।
3. मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की माँग-मूलवासी अपने मूलवास स्थान पर अपना अधिकार चाहते हैं। अपने मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की माँग हेतु सम्पूर्ण विश्व के मूलवासी यह कहते हैं कि हम यहाँ अनन्त काल से निवास करते चले आ रहे हैं।
4. राजनीतिक स्वतन्त्रता की माँग–भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग-अलग स्थानों पर निवास कर रहे हैं, लेकिन भूमि और उस पर आधारित जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि एक-समान है। भूमि की हानि का इनके लिए अर्थ है-आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक स्वतन्त्रता का क्या अर्थ जो जीवन-यापन के साधन ही उपलब्ध न कराए। अत: मूलवासी अपने निवास स्थान पर उपलब्ध संसाधनों पर अपना अधिकार मानते हुए जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।
मूलवासियों के अधिकारों के वैश्विक प्रयास-
मूलवासियों के अधिकारों के लिए वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित प्रयास हए हैं-
- 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में मूलवासियों के प्रतिनिधियों के मध्य सम्पर्क बढ़ा है। इससे इनके साझे अनुभवों एवं सरोकारों को एक आधार मिला है।
- सन् 1995 में मूलवासियों से सम्बन्धित ‘वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इण्डिजिनस पीपल’ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम इस परिषद् को परामर्शदायी परिषद् का दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा आदिवासियों के सरोकारों से सम्बद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा प्रदान किया गया है।
प्रश्न 2.
एजेण्डा-21 से आप क्या समझते हैं? “उत्तरदायित्व संयुक्त, भूमिकाएँ अलग-अलग” का क्या अर्थ है?
उत्तर:
एजेण्डा-21 का अभिप्राय सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केन्द्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो-डी-जनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने हिस्सा लिया। इस . सम्मेलन के दौरान विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला।
इस अवसर पर 21वीं सदी के लिए एक विशाल कार्यक्रम अर्थात् एजेण्डा-21 पारित किया गया। सभी राज्यों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखें, पर्यावरण प्रदूषण को रोकें तथा पोषणीय विकास का रास्ता अपनाएँ।
एजेण्डा-21 के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् थे-
- पर्यावरण एवं विकास के मध्य सम्बन्ध के मुद्दों को समझा जाए।
- ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए।
- किसानों को पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी दी जाए।
- प्रदूषण फैलाने वालों पर भी भारी अर्थदण्ड लगाया जाए।
- इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय योजनाएँ बनाई एवं लागू की जाएँ।
उत्तरदायित्व संयुक्त, भूमिकाएँ अलग-अलग का अर्थ
पर्यावरण एवं संरक्षण को लेकर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अन्तर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामले पर उसी रूप में विचार-विमर्श करना चाहते हैं जिस परिस्थिति में पर्यावरण वर्तमान में विद्यमान है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में प्रत्येक देश का बराबर का उत्तरदायित्व हो।
दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को अधिकांश क्षति (नुकसान) विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंची है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाया है तो इन्हें इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और यह आवश्यक है कि इन पर वे प्रतिबन्ध न लगें जो विकसित देशों पर लगाए जाते हैं।
पृथ्वी सम्मेलन से जुड़े निर्णय अथवा सुझाव
सन् 1992 में सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे ‘संयुक्त उत्तरदायित्व लेकिन अलग-अलग भूमिका का सिद्धान्त’ कहा गया। इस सन्दर्भ में रियो घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “पृथ्वी के पारिस्थितिकी तन्त्र की अखण्डता तथा गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बन्धुत्व की भावना से परस्पर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न राज्यों के अलग-अलग उत्तरदायित्व होंगे। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव अधिक है तथा इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ विकास के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम में विकसित देश अपना विशेष उत्तरदायित्व स्वीकारते हैं।”
प्रश्न 3.
देवस्थान क्या हैं? भारत में पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्त्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा पावन वन-प्रान्तर क्या है? पर्यावरणीय दृष्टि से इसके महत्त्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
पावन वन-प्रान्तर (देवस्थान) का अर्थ
अनेक पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का प्रचलन है। भारत में विद्यमान पावन वन-प्रान्तर इस चलन के सुन्दर उदाहरण हैं। पावन वन-प्रान्तर प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इसे ही पावन वन-प्रान्तर या देवस्थान कहा जाता है।
पावन वन-प्रान्तर (देवस्थान) का देशव्यापी विस्तार भारत में पावन वन-प्रान्तर का देशव्यापी विस्तार पाया जाता है। इनके देशव्यापी विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सम्पूर्ण देश की भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होता है। इन देवस्थानों को राजस्थान में वानी, केंकड़ी व ओसन; मेघालय में लिंगदोह; केरल में काव; झारखण्ड में जहेरा थान व सरना; उत्तराखण्ड में थान या देवभूमि तथा महाराष्ट्र में देवरहतिस आदि नामों से जाना जाता है।
पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पावन वन-प्रान्तर का महत्त्व
पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पावन वन-प्रान्तर के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है-
1. समुदाय आधारित संसाधन प्रबन्धन में महत्त्व–पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित भारतीय साहित्य में पावन वन-प्रान्तर के महत्त्व को अब स्वीकार किया जा रहा है तथा इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबन्धन के रूप में देखा जा रहा है।
2. पारिस्थितिकी तन्त्र के सन्तुलन में महत्त्व-पावन वन-प्रान्तर को हम एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसमें प्राचीन समाज प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तन्त्र का सन्तुलन बना रहे। कुछ शोधकर्ताओं का विश्वास है कि पावन वन-प्रान्तर (देवस्थान) की मान्यता से जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं सांस्कृतिक वैविध्य को बनाए रखने में भी सहायता मिल सकती है।
3. साझी सम्पदा के संरक्षण की व्यवस्था के समान–पावन वन-प्रान्तर की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर-तरीकों से सम्पन्न हैं और इस व्यवस्था की विशेषताएँ साझी सम्पदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती-जुलती हैं।
4. क्षेत्र की आध्यात्मिक या सांस्कृतिक विशेषताएँ-देवस्थान के महत्त्व का परम्परागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं। हिन्दू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ व वन-प्रान्सर भी शामिल हैं। अनेक मन्दिरों का निर्माण, देवस्थान में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता बनाए रखी। पावन वन-प्रान्तर की वर्तमान स्थिति-पिछले कुछ वर्षों से मनुष्यों की बसावट के विस्तार ने धीरे-धीरे पावन वन-प्रान्तर (देवस्थानों) पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। नवीन राष्ट्रीय वन नीतियों के लागू होने के साथ कई स्थानों पर इन परम्परागत वनों की पहचान मन्द पड़ने लगी है। देवस्थान के प्रबन्धन में एक कठिन समस्या यह आ रही है कि देवस्थान का कानूनी स्वामित्व तो राज्यों के पास है तथा इसका व्यावहारिक नियन्त्रण समुदायों के पास है। राज्यों व समुदायों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं एवं देवस्थानों के उपयोग के उद्देश्य में भी इनके बीच कोई तालमेल नहीं है।
इस तरह कहा जा सकता है कि पावन वन-प्रान्तर (देवस्थान) का हमारे देश में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रश्न 4.
अण्टार्कटिका महादेशीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षण, महत्त्व एवं अण्टार्कटिका पर स्वामित्व सम्बन्धी विवाद को विस्तार से बताइए।
उत्तर:
अण्टार्कटिका विश्व के सात प्रमुख महाद्वीपों में से एक है।
अण्टार्कटिका महाद्वीप के प्रमुख लक्षण (विशेषताएँ)
अण्टार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- अण्टार्कटिका महादेशीय क्षेत्र का विस्तार लगभग 1.40 वर्ग करोड़ किमी में फैला हुआ है।
- विश्व के निर्धन क्षेत्र का 26 प्रतिशत भाग इस महाद्वीप में आता है।
- स्थलीय हिम का 90 प्रतिशत भाग एवं धरती के स्वच्छ जल का 70 प्रतिशत भाग इस महाद्वीप में उपलब्ध है।
- इस महादेश का 3.60 करोड़ वर्ग किमी तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है।
- यह विश्व का सबसे सुदूर ठण्डा एवं झंझावाती प्रदेश है।
- सीमित स्थलीय जीवनं वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तन्त्र अत्यन्त उर्वर है, जिसमें कुछ पादप; जैसे-सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन तथा समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य एवं कठिन वातावरण में जीवन-यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल हैं।
- इस महाद्वीप में समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी–क्रिल मछली भी मिलती है। इस मछली पर अन्य जीवों का आहार निर्भर है।
अण्टार्कटिका महाद्वीप का महत्त्व-अण्टार्कटिका महाद्वीप का महत्त्व निम्नलिखित हैं-
- अण्टार्कटिका महाद्वीप विश्व की जलवायु को सन्तुलित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
- इस महाद्वीपीय प्रदेश की आन्तरिक हिमानी परत ग्रीन हाऊस गैस के जमाव का महत्त्वपूर्ण सूचना स्रोत है।
- इस महाद्वीपीय प्रदेश में जमी बर्फ से लाखों वर्ष पूर्व के वायुमण्डलीय तापमान का पता लगाया जा सकता है।
- इस महाद्वीपीय क्षेत्र में समुद्री पारिस्थितिकी तन्त्र अत्यन्त उर्वर पाया जाता है।
- यह क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसन्धान, मत्स्य, आखेट एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
अण्टार्कटिका क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा – अण्टार्कटिका क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तन्त्र की सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं जिनको अपनाया गया है। ये नियम कल्पनाशील एवं दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अण्टार्कटिका एवं पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों में आते हैं। सन् 1959 के पश्चात् इस क्षेत्र में गतिविधियाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान, मत्स्य, आखेट एवं पर्यटन तक ही सीमित रही हैं, लेकिन न्यून गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ भागों में अवशिष्ट पदार्थों जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं।
अण्टार्कटिका पर स्वामित्व-विश्व के सबसे सुदूर ठण्डे एवं झंझावाती महादेश अण्टार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? इसके सम्बन्ध में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश, जैसे—ब्रिटेन, अर्जेण्टीना, चिली, नार्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड ने अण्टार्कटिका क्षेत्र पर अपने सम्प्रभु अधिकार का दावा किया है, जबकि अन्य अधिकांश देशों का मत है कि अण्टार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी सम्पदा है और यह किसी भी राष्ट्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
प्रश्न 5.
पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर भारतीय पक्ष की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर भारतीय पक्ष पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर भारतीय पक्ष की व्याख्या निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा की जा सकती है-
1. भारतीय पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व संयुक्त है, लेकिन भूमिकाएँ अलग-अलग होनी चाहिए-पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरणीय मुद्दे पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण वर्तमान में विद्यमान है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरणीय संरक्षण में प्रत्येक देश का उत्तरदायित्व एक समान हो। दक्षिण के देशों का अभिमत है कि विश्व में पारिस्थितिकी को क्षति अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुई है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक क्षति पहुँचायी है तो उन्हें इसकी भरपाई भी अधिक चाहिए।
2. उत्तरदायित्व को लागू करने हेतु भारतीय सुझाव-इस सन्दर्भ में निम्नलिखित दो सुझाव दिए गए-
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग तथा व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।
- प्रत्येक राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय का कुछ प्रतिशत भाग अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए तथा वह धनराशि सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर विश्व बैंक अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था के माध्यम से मानवीय सुरक्षा एवं संयुक्त सम्पदा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए खर्च की जानी चाहिए।
3. वन संरक्षण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण-दक्षिणी गोलार्द्ध देशों के वन आन्दोलन उत्तरी देशों के वन आन्दोलन से विशेष अर्थों में अलग हैं। दक्षिणी देशों में वन निर्जन नहीं हैं, जबकि उत्तरी गोलार्द्ध के देशों में वन जनविहीन हैं। इसी कारण उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि की श्रेणी में रखा गया है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण पर्यावरण को व्यक्ति से दूर की वस्तु मानता है।
4. पृथ्वी को बचाने हेतु भारतीय सुझाव-इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय हैं-
- पृथ्वी को बचाने हेतु विभिन्न देश सुलह एवं सहकार की नीति अपनाएँ, क्योंकि पृथ्वी का सम्बन्ध किसी एक देश विशेष से न होकर, सम्पूर्ण विश्व एवं मानव जाति से है।
- अभी कुछ समयावधि पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में यह परिचर्चा हुई कि तीव्रता से औद्योगिक विकास करते हुए ब्राजील, चीन तथा भारत इत्यादि देश नियमाचार की बाध्यताओं का परिपालन करते हुए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करें। भारत इस बात के विरुद्ध है और उसकी मान्यता है कि यह तथ्य इस नियमाचार की मूल भावना के विपरीत है।
- हमारे देश भारत पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध थोपना भी अनुचित ही है। सन् 2030 तक भारत में कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के वर्तमान औसत अर्थात् 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। जहाँ सन् 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्जर्सन 0.9 टन था वहीं एक अनुमान के अनुसार सन् 2030 तक यह आँकड़ा बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा।
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
वैश्विक राजनीति में पर्यावरण महत्त्व के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
वैश्विक राजनीति में पर्यावरणीय महत्त्व के प्रमुख मुद्दे निम्नवत् हैं-
(1) विश्व में अब भूमि का विस्तार करना असम्भव है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता लगातार कम होती चली जा रही है। जहाँ चरागाहों के चारे समाप्त होने के कगार पर हैं वहीं मछली भण्डार भी निरन्तर कम होता जा रहा है। इसी तरह जलाशयों का जल-स्तर भी तेजी से घटा है और जल प्रदूषण बढ़ गया है। खाद्य उत्पादों में भी लगातार कमी होती चली जा रही है।
(2) सन् 2006 में जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की एक अरब बीस करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता तथा यहाँ की दो अरब साठ करोड़ की आबादी साफ-सफाई की सुविधा से वंचित है। उक्त कारण से लगभग तीस लाख से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष असमय काल के ग्रास में समा जाते हैं।
(3) वनों की कटाई से लोग विस्थापित हो रहे हैं। वनों की कटाई का प्रभाव जैव प्रजातियों पर भी पड़ा है और अनेक जीव-जन्तु एवं पेड़-पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।
(4) पृथ्वी के ऊपरी वायुमण्डल में ओजोन की मात्रा लगातार घट रही है जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी तन्त्र तथा मानवीय स्वास्थ्य पर गम्भीर संकट आ गया है।
प्रश्न 2.
पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण बताइए।
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- पश्चिमी विचारधारा–पर्यावरण प्रदूषण के लिए पश्चिमी चिन्तन तथा उनकी भौतिक जीवन दृष्टि काफी सीमा तक उत्तरदायी है।
- जनसंख्या में वृद्धि-जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण बढ़ता है तथा पर्यावरण प्रदूषित होता है।
- वनों की कटाई एवं भूक्षरण–वनों की निरन्तर कटाई के फलस्वरूप कार्बन डाइ-ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
- जल प्रदूषण-कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायनों तथा नगरों के गन्दे पानी से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है।
प्रश्न 3.
पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख उपाय लिखिए।
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं-
- समग्र चिन्तन की आवश्यकता-पश्चिमी जगत् के भौतिक चिन्तन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि पृथ्वी पर व प्रकृति पर जो कुछ भी है, वह मानव के उपभोग के लिए है। अत: आवश्यकता मानव की सोंच बदलने की है। इसके लिए भारत का समग्र चिन्तन आवश्यक है।
- वन संरक्षण-पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वनों की अन्धाधुन्ध कटाई को रोकना अति आवश्यक है।
- जनसंख्या नियन्त्रण-पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या को नियन्त्रित करना आवश्यक है।
- वन्य जीव का संरक्षण-पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वन संरक्षण के साथ-साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी किया जाए।
प्रश्न 4.
पर्यावरण के सन्दर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं?
उत्तर:
पर्यावरण के सन्दर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा निम्न प्रकार कर सकते हैं-
- मूलवासियों के प्राकृतिक आवास अर्थात् वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।
- आदिवासियों को उनकी परम्परा में परिवर्तन किए बिना मूल रूप से राजनीतिक संरक्षण दिया जाए।
- आदिवासियों (मूलवासियों) को संगठित करके विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दिलाया जाए।
- आदिवासियों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्गदर्शन देकर मुख्यधारा के साथ जुड़ने की उनमें स्वतः इच्छा जाग्रत की जाए।
प्रश्न 5.
यू०एन०ई०पी० क्या है? इसके किन्हीं दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
यू०एन०ई०पी० संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से सम्बद्ध (जुड़ी) एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी या संस्था है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन्स एनवायरमेण्ट प्रोग्राम (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) है। इसके दो प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं-
- संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात् यूनाइटेड नेशन्स एनवायरमेण्ट प्रोग्राम सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराया और इस विषय के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
- इस संस्था का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से प्रयासों की अधिक कारगर विश्व स्तर पर शुरुआत करना था। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन सका।
प्रश्न 6.
पर्यावरण से सम्बन्धित उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों के विचारों में क्या अन्तर है?
उत्तर:
इस तथ्य को हम निम्नलिखित दो बिन्दुओं द्वारा सरलता से स्पष्ट कर सकते हैं-
(1) जहाँ उत्तरी गोलार्द्ध के देश वन क्षेत्र को बीहड़ या जनहीन प्रान्त मानते हैं वहीं दक्षिणी गोलार्द्ध के देश इनको देवस्थान या वन-प्रान्तर स्थान जैसे श्रद्धा उत्पन्न करने वाले नामों से पुकारते हैं। जब वनों के प्रति विकसित देशों अर्थात् उत्तरी गोलार्द्ध की धारणा ही तुच्छ कोटि की है, जबकि पर्यावरणीय एजेण्डा-21 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण अथवा मानवता की संयुक्त विरासत को विनाश से बचाने की उनकी अधिक जिम्मेदारी रहेगी। उन्हें अपनी धारणा के साथ-साथ कार्यप्रणाली में भी आमूल-चूल बदलाव लाना है।
(2) दक्षिणी गोलार्द्ध का पर्यावरणीय एजेण्डा ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा कम दर्शाता है जबकि उत्तरी गोलार्द्ध का एजेण्डा इन्हें अधिक दर्शाता है।
प्रश्न 7.
क्योटो प्रोटोकॉल का क्या महत्त्व है? क्या भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
उत्तर:
क्योटो प्रोटोकॉल को पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप मान्यता मिली। औद्योगिक विकास से सम्पन्न देश पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने पर सहमत हुए। ऐसे विकसित उत्तरी गोलार्द्ध के देश अपने कल-कारखानों से निकलने वाली हरित प्रभाव गैसों का अनुपात घटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे।
इस अन्तर्राष्ट्रीय सहमति पर जापानी शहर क्योटो में सन् 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के दौरान यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) द्वारा निर्धारित मापदण्डों को स्वीकार कर लिया गया था। अगस्त 2002 में भारत ने इस न्यायाचार को हस्ताक्षरित किया। इसके अनुसार चीन सहित भारत को विकासशील देश मानते हुए हरित गैसों की मात्रा घटाने के दायित्व से मुक्त रखा गया। उल्लेखनीय है कि इन देशों के औद्योगिक विकास से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण को उतनी हानि नहीं हुई है, जितनी कि पश्चिमी तथा अन्य औद्योगिक विकसित राष्ट्रों में हुई।
प्रश्न 8.
ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को नियन्त्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए किन्हीं पाँच प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को नियन्त्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए अग्रलिखित पाँच प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-
- भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को सन् 2002 में हस्ताक्षरित करके उसका अनुमोदन किया है।
- भारत ने अपनी राष्ट्रीय मोटर-कार ईंधन नीति में वाहनों के लिए स्वच्छत्तर ईंधन अनिवार्य कर दिया है।
- सन् 2001 में पारित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 में प्राकृतिक गैस के आयात, अपूरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया है।
- भारत बायोडीजल से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी प्रयासरत है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
आप पर्यावरण आन्दोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कथनों को उठाएँगे?
उत्तर:
- पर्यावरण आन्दोलन के स्वयंसेवक के रूप में हम वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के विरुद्ध आन्दोलन चलाएँगे तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे।
- खनिजों के अन्धाधुन्ध दोहन के विरोध में आन्दोलन करेंगे।
प्रश्न 2.
पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित स्टॉकहोम सम्मेलन के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण सम्मेलन जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु सात महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया।
प्रश्न 3.
क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के सम्मेलन का आयोजन जापान के क्योटो शहर में 1 दिसम्बर से 11 दिसम्बर, 1997 तक हुआ। इस सम्मेलन में कहा गया कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश सन् 2008 से 2012 तक सन् 1990 के स्तर से नीचे 5.2% तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी करेंगे।
प्रश्न 4.
माण्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए।
उत्तर:
सन् 1987 में 175 औद्योगिक देशों ने माण्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ओजोन परत को बचाने के लिए यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सहमति थी जिसे माण्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- ओजोन ह्रास करने वाले पदार्थों के उत्पादन में कमी लाना।
- ओजोन ह्रास वाले पदार्थों के विकल्प ढूँढना।
- ओजोन उत्पादन पर नियन्त्रण करना।
प्रश्न 5.
विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
सन् 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण तथा संसाधन प्रबन्ध के समाधान के सम्बन्ध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार की सम्भावनाओं पर विचार किया गया।
प्रश्न 6.
विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है?
उत्तर:
कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं; जैसे—पृथ्वी का वायुमण्डल, अण्टार्कटिका, समुद्री सतह तथा बाहरी अन्तरिक्ष आदि। इसका प्रबन्धन अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है। इन्हीं को ‘विश्व की साझी विरासत’ या ‘साझी सम्पदा’ कहा जाता है।
प्रश्न 7.
विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के कोई दो उपाय बताइए।
उत्तर:
विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं-
- सीमित प्रयोग-विश्व की साझी विरासतों का सीमित प्रयोग करना चाहिए।
- जागरूकता पैदा करना—विश्व की साझी विरासतों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
प्रश्न 8.
ब्यूनस आइरस सम्मेलन कब और क्यों हुआ?
उत्तर:
अर्जेण्टीना के ब्यूनस आइरस में जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फेमवर्क कन्वेंशन से सम्बद्ध पक्षों का चौथा अधिवेशन 2 नवम्बर से 14 नवम्बर, 1998 को हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन क्योटो, प्रोटोकॉल 1997 के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए किया गया था।
प्रश्न 9.
पर्यावरण सम्बन्धी नियमों को समकालीन विश्व राजनीति के हिस्से के रूप में क्यों देखना चाहिए?
उत्तर:
पर्यावरण के वर्तमान में हो रहे विनाश को कोई एक सरकार नहीं बल्कि समूचे विश्व की सरकारें ही विचार-विमर्श करके रोक सकती हैं। इस दृष्टि से पर्यावरण सम्बन्धी नियमों को समकालीन विश्व राजनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रश्न 10.
मूलवासियों को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:
मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूद देश में लम्बी समयावधि से रहते चले आ रहे हैं। यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनको अपने अधीन कर लिया तथापि ये अभी भी अपनी परम्परा, संस्कृति, रीति-रिवाज का पालन करना पसन्द करते हैं।
प्रश्न 11.
मूलवासियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मूलवासियों के अधिकार निम्नलिखित हैं-
- विश्व में मूलवासियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो।
- मूलवासियों को अपनी स्वतन्त्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए।
- मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न किया जाए।
- देश के विकास से होने वाला लाभ मूलवासियों को भी मिलना चाहिए।
प्रश्न 12.
विश्व नेताओं ने भूमि पर्यावरण की चिन्ता क्यों की? कारण बताइए।
उत्तर:
विश्व नेताओं द्वारा भूमि पर्यावरण की चिन्ता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- विश्व में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता कम हो रही है।
- जलाशयों में प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है।
प्रश्न 13.
समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण किस कारण से बढ़ रहा है?
उत्तर:
समुद्रतटीय क्षेत्रों का जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्रतटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है यदि इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।
प्रश्न 14.
वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिन्ता के कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिन्ता के कारण निम्नलिखित हैं-
- वनों की अन्धाधुन्ध कटाई-दक्षिण देशों में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई से जलवायु, जल चक्र असन्तुलित हो रहा है तथा जैव विविधता खत्म हो रही है।
- ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन-ग्रीन हाऊस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत के क्षीण होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मँडरा रहा है।
प्रश्न 15.
पर्यावरण से सम्बन्धित भारत सरकार के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
भारत सरकार ने पर्यावरण से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रयास किए-
- भारत ने अपनी ‘नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी’ में वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया।
- सन् 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल के लिए ‘प्रतिबद्धता प्रकट की गई है।
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है-
(a) वायुमण्डल
(b) सड़क मार्ग
(c) समुद्री सतह
(d) बाहरी अन्तरिक्षा
उत्तर:
(b) सड़क मार्ग।
प्रश्न 2.
क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ वह है-
(a) जापान
(b) सिंगापुर
(c) नेपाल
(d) बाली।
उत्तर:
(a) जापाना

प्रश्न 3.
रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया-
(a) 172
(b) 170
(c) 180
(d) 185
उत्तर:
(b) 170
प्रश्न 4.
पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का कारण है-
(a) पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जारी है।
(b) विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिन्तित हैं।
(c) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक
पहुँच गया है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
उत्तर:
(c) मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुँच गया है।
प्रश्न 5.
पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ—
(a) 1992 में
(b) 1995 में
(c) 1997 में
(d) 2000 में।
उत्तर:
(a) 1992 में।
प्रश्न 6.
माण्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए-
(a) 170
(b) 172
(c) 175
(d) 180
उत्तर:
(c) 175
प्रश्न 7.
धरती के वायुमण्डल में निम्नलिखित में से जिस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, वह है-
(a) ओजोन गैस
(b) कार्बन डाइ-ऑक्साइड गैस
(c) मीथेन गैस
(d) नाइट्रस ऑक्साइड गैस।
उत्तर:
(a) ओजोन गैस।
प्रश्न 8.
भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया-
(a) सन् 1997 में
(b) सन् 1998 में
(c) सन् 2002 में
(d) सन् 2001 में।
उत्तर:
(c) सन् 2002 में।
![]()


![]()

![]()
![]()
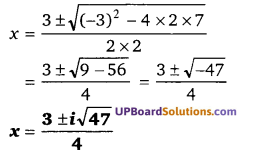
![]()
![]()
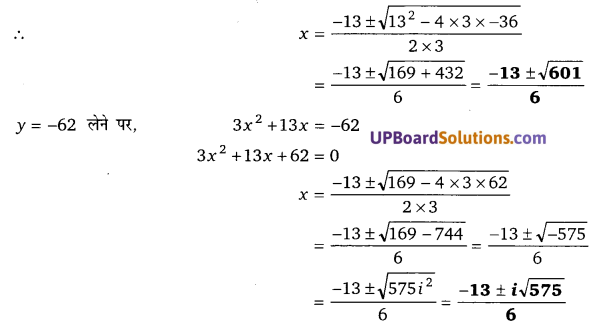
![]()

![]()
![]()