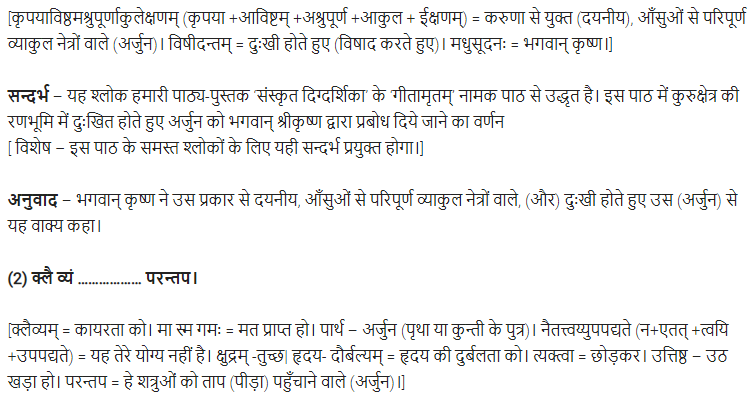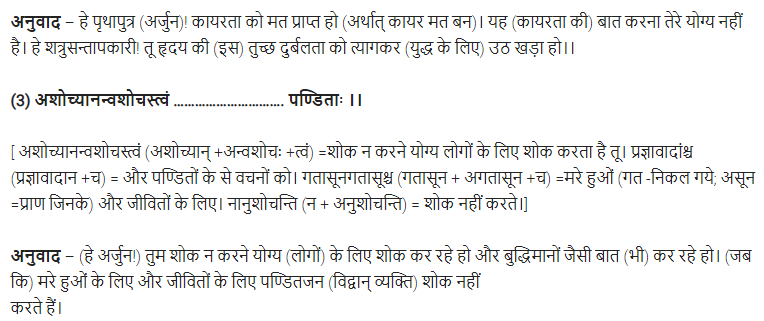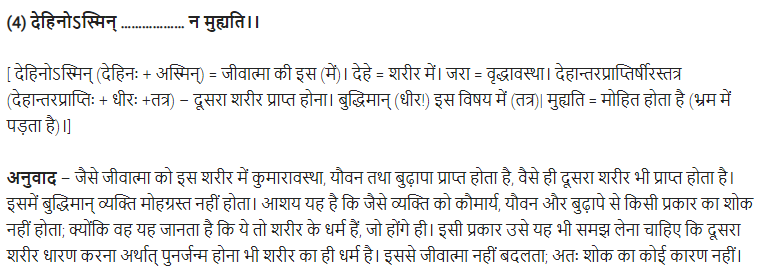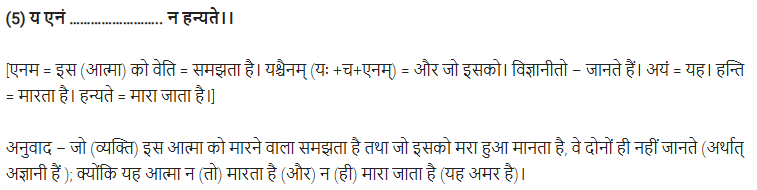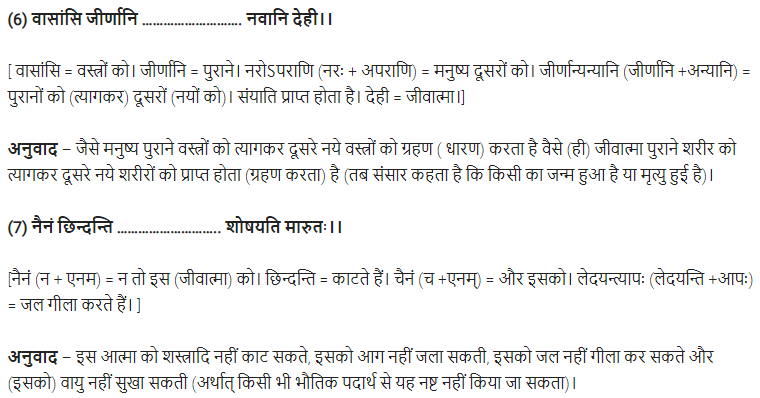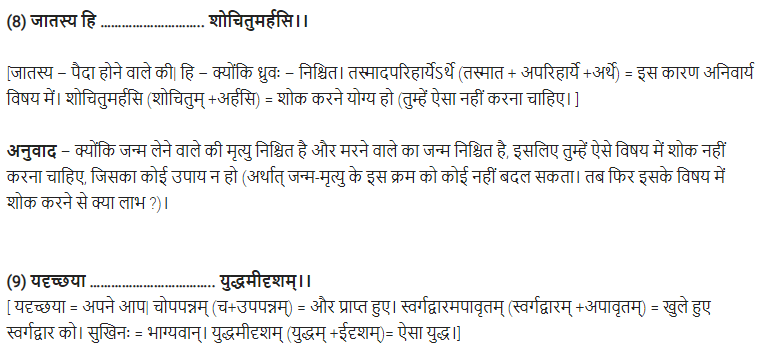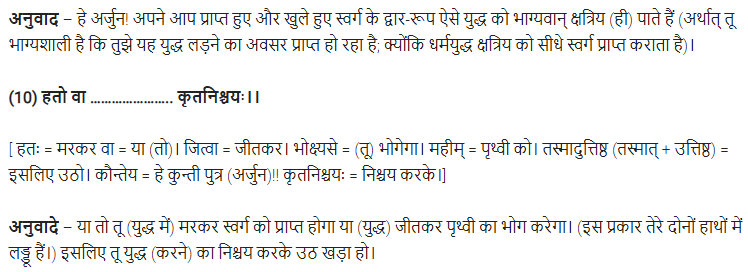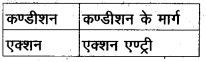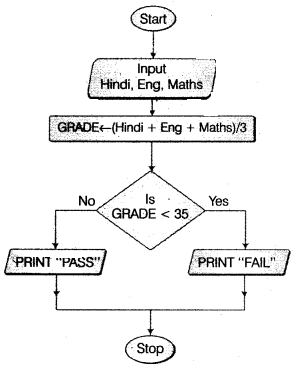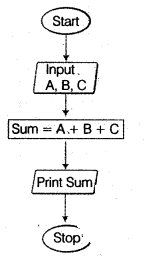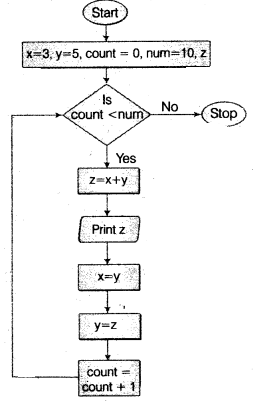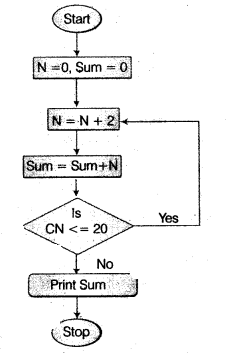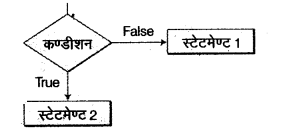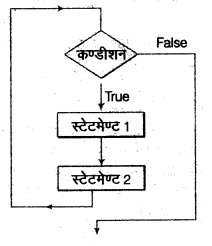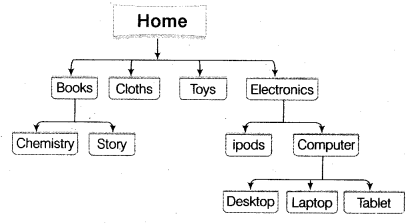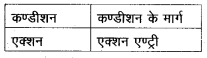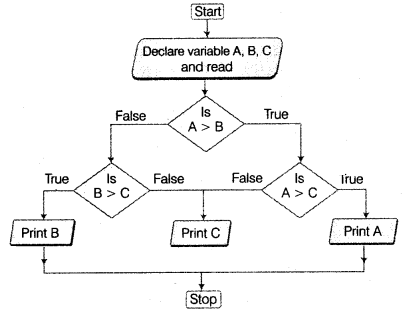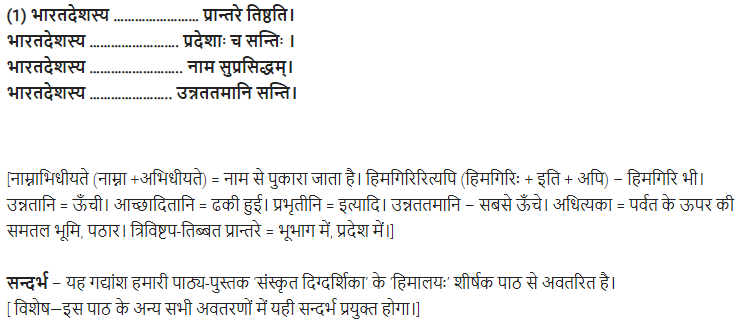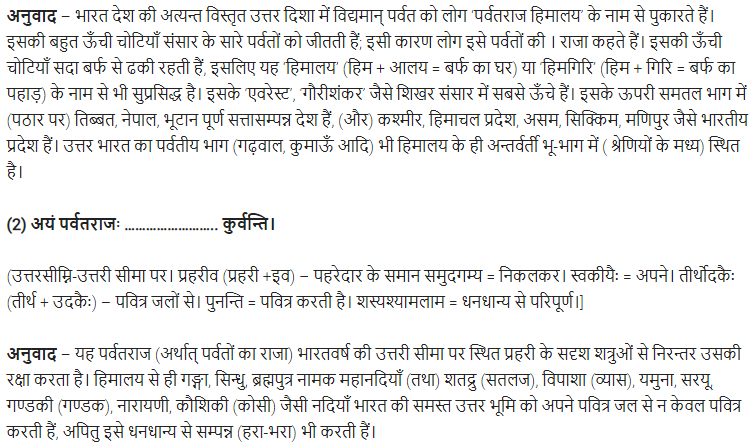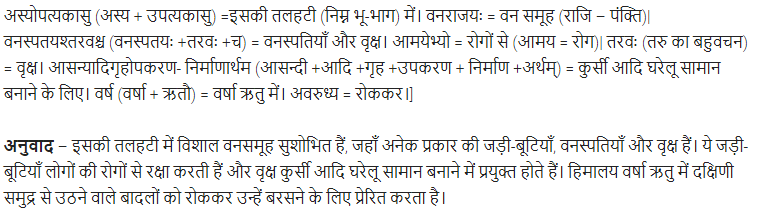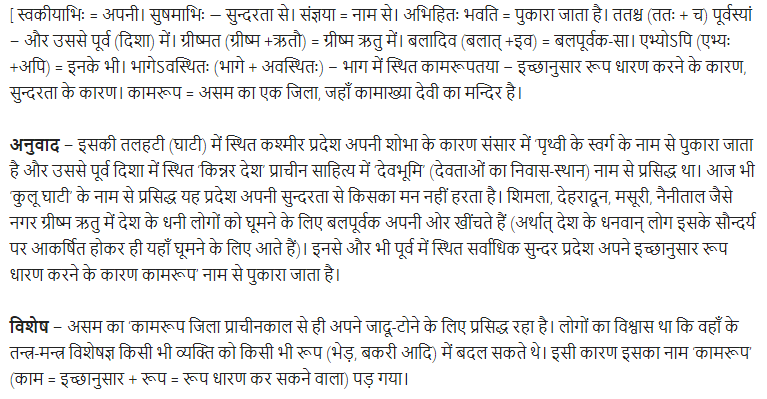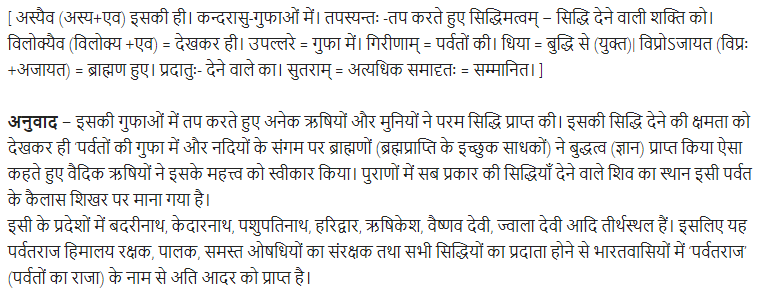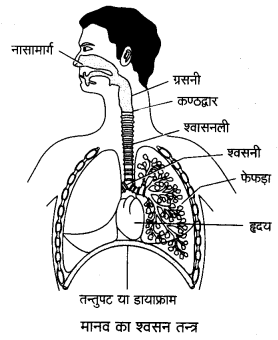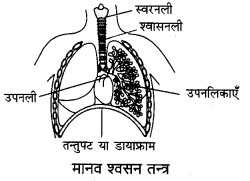UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 1 पोषण एवं सन्तुलित आहार are part of UP Board Solutions for Class 12 Home Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 1 पोषण एवं सन्तुलित आहार.
| Board |
UP Board |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Home Science |
| Chapter |
Chapter 1 |
| Chapter Name |
पोषण एवं सन्तुलित आहार |
| Number of Questions Solved |
22 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 1 पोषण एवं सन्तुलित आहार
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
सन्तुलित आहार के पोषक तत्वों में से कौन-सा तत्त्व सम्मिलित नहीं है?
(a) प्रोटीन
(b) कार्बोहाइड्रेट
(C) खनिज लवण
(d) पोषण
उत्तर:
(d) पोषण
प्रश्न 2.
पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है?
(a) प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर
(b) शरीर निर्माणक पोषक तत्वों के आधार पर
(c) जलवायु परिवर्तन के आधार पर
(d) आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर
उत्तर:
(b) शरीर निर्माणक पोषक तत्वों के आधार पर
प्रश्न 3.
किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों को क्रमशः कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं?
(a) 2650 से 2080 कैलोरी ऊर्जा
(b) 2250 से 2600 कैलोरी ऊर्जा
(c) 2600 से 2800 कैलोरी ऊर्जा
(d) 2400 से 2800 कैलोरी ऊर्जा
उत्तर :
(a) 2650 से 2080 कैलोरी ऊर्जा
प्रश्न 4.
रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
(a) विटामिन A
(b) विटामिन C
(c) विटामिन K
(d) विटामिन D
उत्तर:
(a) विटामिन A
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक, 25 शब्द
प्रश्न 1.
सन्तुलित आहार का क्या अर्थ है?
उत्तर:
वह आहार जो मनुष्य की पोषण सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सन्तुलित आहार कहलाता है।
प्रश्न 2.
सन्तुलित आहार के पोषक तत्वों का नाम बताइए।
उत्तर:
सन्तुलित आहार के पोषक तत्त्व निम्नलिखित हैं
- कार्बोहाइड्रेट
- वसा एवं तेल
- प्रोटीन
- विटामिन
- खनिज लवण
- जल आदि।
प्रश्न 3.
सन्तुलित आहार का महत्त्व बताइए।
उत्तर:
सन्तुलित आहार शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। इसके अभाव में शारीरिक व मानसिक विकास उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाता है।
प्रश्न 4.
दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों माना गया है?
उत्तर:
पोषण में दुग्ध को सम्पूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया है। दूध ही एकमात्र ऐसा भोज्य पदार्थ है, जिसका स्थान अन्य कोई भोज्य पदार्थ नहीं ले सकता। दूध शिशुओं के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है।
प्रश्न 5.
आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है?
उत्तर:
घेघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है।
प्रश्न 6.
वसा की अधिकता से कौन-सा रोग होता है?
उत्तर:
वसा की अधिकता से मोटापा हो जाता है, इसके अतिरिक्त इससे उच्च रक्त चाप रोग भी हो जाता है।
प्रश्न 7.
सन्तुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
सन्तुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक आयु, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता तथा विशेष शारीरिक अवस्था आदि हैं।
प्रश्न 8.
लकवा किस विटामिन की कमी से होता है?
उत्तर:
विटामिन B1 की कमी से शरीर में लकवा (Paracysis) की शिकायत हो जाती है।
लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, 50 शब्द
प्रश्न 1.
सन्तुलित आहार से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। वायु और जल के पश्चात् हमारे लिए भोजन ही सबसे आवश्यक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्त्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में और साथ ही शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। सन्तुलित आहार के अभाव में मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
प्रश्न 2.
नवजात शिशु के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिए सन्तुलित आहार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर:
प्रत्येक प्राणी के लिए सन्तुलित आधार की मात्रा का निर्धारण अलग-अलग होता है, जो निम्न प्रकार से है
- नवजात शिशु के लिए आहार माँ का दूध नवजात शिशु के लिए एक सर्वोत्तम आहार है। यह शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि तथा जीवन शक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है, क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक तत्त्व; जैसे—प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, लवण, जल तथा विटामिन (B,D) उपस्थित होते हैं।
- स्कूली बच्चों का आहार स्कूल जाने वाले बच्चों को अधिक मात्रा में | प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की वृद्धि की दर भी बढ़ती रहती है। इन बच्चों को आहार में प्रोटीन, विटामिन, दूध, सब्जियाँ, फल एवं अण्डे आदि पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए।
प्रश्न 3.
किशोरावस्था, वयस्क पुरुष व महिला तथा प्रौढ़ावस्था के लिए सन्तुलित आहार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर:
प्रत्येक अवस्था में सन्तुलित आहार का निर्धारण अलग-अलग होता है, जो निम्न प्रकार से है
- किशोरावस्था में आहार किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियों को क्रमशः 2650 से 2080 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं।
- वयस्क पुरुष व महिला का आहार एक वयस्क पुरुष को महिलाओं की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें महिलाओं की अपेक्षा अधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने होते हैं, किन्तु गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को वयस्क पुरुषों के समान ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है।
- प्रौढावस्था में आहार इस अवस्था में शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवस्था 45 वर्ष के पश्चात् आती है। इस अवस्था में शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं तथा पाचन संस्थान कमजोर होने लगता हैं।
प्रश्न 4.
पोषक तत्वों की कमी से होने वाली कोई दो बीमारियों के बारे में बताइए।
उत्तर:
पोषक तत्वों की कमी से होने वाली दो बीमारियाँ निम्न प्रकार हैं
1. रक्ताल्पता रक्ताल्पता (एनीमिया) से आशय खून की कमी से होता है।यदि मानव शरीर में लौह खनिज की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में रक्ताल्पता नामक बिमारी हो जाती है। यह लौह युक्त भोजन (आहार) के अभाव में होता है। थकान या कमजोरी महसूस करना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस बिमारी के कारण मानव शरीर में जैविक क्रिया, पाचन क्रिया आदिप्रभावित होती हैं।
2. मरास्मस मरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है- व्यर्थ करना। इस बिमारी से अधिकांशतः बच्चे ग्रसित है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मरास्मस रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारहीनता, रक्तहीनता, त्वचा का झुरींदार होना, पेचिश(दस्त) आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
प्रश्न 5.
पोषक तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
पोषक तत्त्व वह रसायन होता है, जिसकी आवश्यकता किसी जीव को उसके जीवन और वृद्धि के साथ-साथ उसके शरीर की उपापचय की क्रिया संचालन के लिए आवश्यक होता है और जिसे वह अपने वातावरण से ग्रहण करता है। पोषक तत्व जो शरीर को समृद्ध बनाते हैं। ये ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं साथ ही शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है।
पोषक तत्वों का प्रभाव मानव द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर निर्भर करता है। इन सभी के अतिरिक्त एक और पोषक तत्त्व है, जिसकी हमारे शरीर को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता होती है, वह है-सेल्युलोज। यह हमारे शरीर में मेल को गति प्रदान करता है तथा आँतों में क्रमांकुचन की गति को सामान्य बनाए रखता है। यह पौष्टिक तत्त्व हमें सब्जियों व फलों के छिलके, साबुत दालों व अनाजों तथा चोकर आदि से प्राप्त होते हैं। जानवरों में विशेष रूप से इसे पचाने वाला एंजाइम होता है।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक, 100 शब्द
प्रश्न 1.
सन्तुलित आहार क्या है? सन्तुलित आहार को प्रभावित करने वालेकारक लिखिए।
उत्तर:
सन्तुलित आहार
भोजन हमारे शरीर का मूल आधार है। विभिन्न खाद्य पदार्थों, जिनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्त्व निहित होते हैं, के मिश्रण से बना वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्त्व सही अनुपात में प्रदान करे, सन्तुलित आहार कहलाता है। सन्तुलित आहार शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्त्व प्रदान करता है, जो शरीर में आवश्यकतानुसार स्वयं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उपयुक्त हो जाते हैं।
सन्तुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक
सन्तुलित आहार अनेक प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं।
1. आयु सन्तुलित आहार को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक ‘आयु’ है। बाल्यावस्था में शारीरिक निर्माण व विकास के लिए सन्तुलित आहार की आवश्यकता आयु के अन्य स्तरों में अधिक होती है।
बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक भोज्य तत्त्वों की आवश्यकता होती है।
बाल्यावस्था में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि वृद्धावस्था में शरीर संवदेनशील होने के कारण, सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती हैं।
2. लिंग स्त्रियों एवं पुरुषों के सन्तुलित आहार में अन्तर होता है। पुरुषों में आकार, भार तथा क्रियाशीलता अधिक होने के कारण महिलाओं की अपेक्षा ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इन कारणों से हुई शारीरिक टूट-फूट अधिक होने के कारण पुरुषों को सुरक्षात्मक तत्त्वों की भी अधिक आवश्यकता होती है, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में यथा गर्भावस्था व दुग्धपान की अवस्थाओं में स्त्रियों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
3. स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार भी पोषक तत्त्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को सन्तुलित आहार की आवश्यकता केवल उसकी दिनचर्या उचित प्रकार से चलाने के लिए चाहिए, परन्तु एक अस्वस्थ व्यक्ति को सन्तुलित आहार की आवश्यकता शरीर की दैनिक दिनचर्या के साथ-साथ टूटे-फूटे ऊतकों आदि की मरम्मत के लिए भी होती है।
4. क्रियाशीलता व्यक्ति की क्रियाशीलता भी उसके सन्तुलित आहार की आवश्यकता को निर्धारित करती है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति को कम क्रियाशील व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
5. जलवायु जलवायु तथा मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करते हैं।ठण्डे देश के निवासी ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर का ताप बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी कारण उन्हें अधिक सन्तुलित आहार की आवश्यकताहोती है।
6. विशेष शारीरिक अवस्था कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाएँ; जैसेगर्भावस्था, दुग्धपान की अवस्था, ऑपरेशन के बाद की अवस्था, जल जाने के बाद की अवस्था तथा रोग के उपचार होने के बाद स्वस्थ होने की अवस्था आदि में सन्तुलित आहार की आवश्यकता बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण निर्माण के कारण एवं माता के शारीरिक भार में परिवर्तन के कारण पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। दुग्धपान की अवस्था में लगभग 400 से 500 मिली दूध के निर्माण के कारण माता में सन्तुलित आहार की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑपरेशन तथा जले जाने के बाद की अवस्था में भी निर्माणक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है।
प्रश्न 2.
सन्तुलित आहार की अर्थ बताइए व उसके आयोजन में ध्यान रखने योग्य बातें बताइट।
उत्तर:
सन्तुलित आहार का अर्थ इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 देखें।
सन्तुलित आहार का आयोजन
परिवार के सभी सदस्यों की सन्तुलित आहार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सन्तुलित आहार का आयोजन करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।
- भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्त्वों; जैसे-कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल आदि तत्त्वों का सामावेश प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतानुसार होना आवश्यक है। किसी भी पोषक तत्त्व की न्यूनतम मात्रा के साथ साथ अधिकतम मात्रा भी समान रूप से हानिकारक होती हैं।
- भोजन का निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी खाद्य पदार्थ पूर्णतः पक जाएँ, तभी वह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे। कम पका हुआ। व अधिक पका हुआ दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।
- भोजन में प्रतिदिन विविधता होना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के पोषक.तत्त्वों की आपूर्ति हो सके।
- व्यक्ति को प्राय: ताजा भोजन ही आहार के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अधिक समय का पका हुआ भोजन विषैला व दुर्गन्ध युक्त हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के विकार के उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
प्रश्न 3.
विभिन्न पोषक तत्वों के नाम बताइए तथा उनकी प्राप्ति के स्रोत कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं, उन्हें पोषक तत्त्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्त्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में न हों, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ये आवश्यक तत्त्व जब हमारे शरीर में आवश्यकतानुसार (सही अनुपात में) उपस्थित होते हैं, तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। ये पोषक तत्व निम्नलिखित हैं।
- काबोहाइड्रेट
- वसा एवं तेल
- प्रोटीन
- खनिज लवण
- विटामिन
- जल
पोषकतत्त्वों का वर्गीकरण
कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया। जाता है
- ऊर्जादायक पोषक तत्त्व कार्बोहाइड्रेट, वसा|
- शरीर निर्माणक पोषक तत्त्वं प्रोटीन एवं खनिज लवण।
- शरीर संरक्षक पोषक तत्त्व खनिज लवण एवं विटामिन।
पोषक तत्वों के आहारीय स्रोत
पोषक तत्वों के आहारीय स्रोत निम्न प्रकार से हैं
- कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, साबूदाना, जौ, मैदा, मुरमुरे, चूड़ा, दलिया, बिस्किट, डबल रोटी, गुड़, चीनी, शहद, किशमिश, खजूर, अंजीर, दालें, शकरकन्द, जमींकन्द, अरवी, जैम-जैली, मुरब्बे, मिठाइयाँ आदि।
- वसा एवं तेल घी, मक्खन, मलाई, मार्गरीन, चर्बी, चर्बीयुक्त मांस, अण्डे को पीला भाग, मछली, वनस्पति घी, सभी प्रकार के तिलहन तथा खाने योग्य तेल, नारियल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता इत्यादि।
- प्रोटीन दूध तथा दूध से बनी चीजें, अण्डा, मांस, मछली, यकृत, दालें, फलियाँ, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, काजू, बादाम, तिल इत्यादि।
- खनिज लवण पोषक तत्त्वों के खनिज लवण निम्नलिखित हैं।
- कैल्शियम दूध, दही, अण्डे, पालक, मैथी, बथुआ, प्रत्येका धनिया, पुदीना, सलाद के पत्ते, सूखी मछली, पनीर, खोआ, तिल इत्यादि।
- फास्फोरस दूध, अण्डा, मांस, मछली, पनीर, अनाज, दालें, गिरी, पत्तेदार सब्जियाँ एवं तिलहन।
- लौह-लवण मांस, मछली, अण्डा, यकृत, अनाज, फलियाँ, प्रत्येकी-पत्ती वाली सब्जियाँ, गुड़, किशमिश, खजूर, अंजीर, काष्ठफल इत्यादि।
- पोटैशियम अनाज, दालें, जड़ वाली सब्जियाँ, दूध, दही, छाछ, पनीर, अण्डा, सोयाबीन, मांस, मछली।
- सोडियम नमक, जल एवं लगभग सभी खाद्य पदार्थों में विशेषकरअनाज और प्रत्येक पत्तेदार सब्जियों में।
- आयोडीन जल, प्रत्येके पत्ते वाली सब्जियाँ, मछली व आयोडीनयुक्त नमक।
- विटामिन पोषक तत्वों में विटामिन इस प्रकार हैं
- विटामिन ‘ए‘ मछली के यकृत का तेल, मक्खन, घी, अण्डा, दूध, पपीता, कद्दू, आम आदि।
- विटामिन ‘डी‘ मछली का यकृत, अण्डा, मक्खन, घी, दूध सूर्य की किरणें आदि।
- विटामिन ‘बी‘ (के अन्तर्गत 12 विटामिन आते हैं, जिनमें कुछप्रमुख हैं- बी1, बी2, बी6, बी12) सम्पूर्ण अनाज, खमीर, साबुत तथा छिलके वाली दालें, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, मटर, फलियाँ, मांस, मछली, दूध, अण्डे की जर्दी, पत्तेदार सब्जियाँ आदि।
- विटामिन ‘सी‘ आँवला में (अत्यधिक), अमरूद, नींबू, सन्तरा, रसभरी, अनन्नास, पपीता, टमाटर, सहजन की पत्तियाँ, धनिया, करमी का साग, चौलाई का साग, अंकुरित मूंग, चना आदि।
- विटामिन ‘ई‘ अण्डा, गेहूं, सोयाबीन, तेल आदि ।
- विटामिन ‘के‘ सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, टमाटर, दूध आदि।
प्रश्न 4.
‘दूध एक सम्पूर्ण आहार है। इस कथन की विवेचना कीजिए।
अथवा
दूध सम्पूर्ण आहार है, क्यों?
अथवा
दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
दूध को सम्पूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया है। यह पूर्ण एवं सुपाच्य आहार है। शिशुओं के शारीरिक विकास एवं वृद्धि हेतु उनके सम्पर्क में आने वाला पहला भोज्य पदार्थ दूध ही होता है। शैशवावस्था से लेकर जीवन के प्रत्येक पड़ाव में शारीरिक वृद्धि, विकास एवं संरक्षण हेतु सभी आवश्यक पौष्टिक तत्त्व उचित मात्रा एवं अनुपात में दूध में उपस्थित होते हैं। विभिन्न स्तनधारियों की स्तनग्रन्थि का स्राव ही दूध कहलाता है; जैसे-गाय, भेड़, बकरी, ऊँट आदि।
दूध में अधिकांश मात्रा में जल विद्यमान होता है, जिसकी मात्रा लगभग 87.25% होती है। शेष भाग ठोस पदार्थ होता हैं, जिनमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि होते हैं। कुछ मात्रा में दूध में घुलनशील गैस, एंजाइम तथा रंग कण भी विद्यमान होते हैं।
दूध में पोषक तत्वों का अनुपात
पोषक तत्वों का अनुपात दूध के संगठन में निम्न प्रकार से हैं
1. जल दवा में अधिकांश मात्रा में जल होता है। दूध में लगभग 80-90% जल विद्यमान होता है, जिसमें विभिन्न पोषक तत्त्व निहित होते हैं। ये तत्त्व घुलित अवस्था अथवा पायस अवस्था में जल में पाए जाते हैं।
2. वसा दृध में 3.5% -7.5% तक वसा होती है, जिसका गठन जटिल लिपिड्स के मिश्रण से होता है। दूध का विशेष स्वाद दूध में उपस्थित वसा के कारण ही होता है। दूध में संतृप्त (62%) व असंतृप्त (37%) वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं, जिनमें 426 कार्बन अणु श्रृंखला तक होते हैं। लघु श्रृंखला वाले वसीय अम्ल; जैसे—पारिटिक, ऑलिक और न्यूटायरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसी कारण दूध में विशिष्ट गन्ध व फ्लेवर उत्पन्न होते हैं। वसा पायस के रूप में होने के कारण दूध में सुगमता से पच जाती है। भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होते हैं।
3. प्रोटीन दूध के मुख्य प्रोटीन हैं-केसीन, लैक्टोएल्यूमिन एवं लैक्टोग्लोब्यूलिन। यह प्रोटीन उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है। प्रमुख कार्बोज लैक्टोज शर्करा है। दूध का लैक्टोज शरीर द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। लैक्टोज शर्करा आँत में लैक्टोबेसीलस जीवाणु की क्रिया से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। इसी कारण दूध से दही जमती है। यह आँतों में कोमल दही बनाती है व दूध की सुपाच्यता को बढ़ाती है। Ph को कम करके कैल्शियम सहित अन्य खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। 100 ग्राम दूध में 2.5-3.5 ग्राम प्रोटीन पाई जाती हैं।
4. खनिज तत्व दूध मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस का उत्कृष्ट साधन है। इसका अवशोषण शीघ्रता से शरीर में हो जाता है। कैल्शियम की आवश्यकता आपूर्ति हेतु हमें प्रतिदिन दूध का सेवन करना चाहिए। दूध में लोहा, ताँबा, जस्ता, मैंगनीज, सिलिका तथा सल्फर भी अल्प मात्रा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवणों की मात्रा 0.3% से 0.8% तक होती है।
5. विटामिन दूध में लगभग सभी प्रमुख विटामिन उपस्थित रहते हैं। घुलनशील विटामिन ‘ए’, ‘डी’, ‘इ’ एवं ‘के’ दूध की वसा में पाए जाते हैं। दूध में विटामिन ‘बी’ समूह का भी अच्छा साधन हैं। थायमिन साधारण मात्रा में ही पाया जाता है, परन्तु धूप व रोशनी के सम्पर्क में आने से लगभग आधा राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। दूध में विटामिन ‘सी’ व ‘डी’ अत्यन्त ही न्यून मात्रा में होता है और गर्म करने अथवा वायु के सम्पर्क में आने से नष्ट हो जाता है।
6. एंजाइम एंजाइम भी कुछ मात्रा में दूध में उपलब्ध होते हैं। एंजाइम एक आंगिक उत्प्रेरक है, जोकि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्रता प्रदान करते हैं। इसी कारण ज्यादा देर तक बिना गरम किए दूध को रखने पर वह फट जाता है या खट्टा हो जाता है। दूध में उपस्थित लाइपेज, एंजाइम वसा विघटन में, अमायलेस, काज विघटन में, प्रोटीएस, प्रोटीन विघटन में वे लैक्टोज एंजाइम दूध के लैक्टोज विघटन में सहायक है।
प्रश्न 5.
पोषण को परिभाषित करते हुए कुपोषण के कारण व लक्षण पर प्रकाश डालिए।
अथवा
पोषण व कुपोषण को परिभाषित कीजिए एवं कुपोषण के कारण व लक्षणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
पोषण की परिभाषा देते हुए भोजन के कार्यों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
पोषण का अर्थ एवं परिभाषा
संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीने व अपनी दिनचर्या चलाने के लिए भोजन ग्रहण करता है। उस भोजन की मात्रा प्रत्येक आयु, वर्ग, शारीरिक स्थिति, जलवायु, देश, क्रियाशीलता आदि तत्त्वों से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की माँग, अन्य किसी व्यक्ति से भिन्न होती है।
पोषण विज्ञान द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमें अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें उस आहार में निहित पोषक तत्त्वों का पूर्ण लाभ मिल सके। आहार विज्ञान पोषण विज्ञान को प्रायोगिक तरीके से अपनाने का ज्ञान प्रदान करता है। अतः इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त आहार नियोजन कर सकता है।
टर्नर के अनुसार, “पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है, जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है व उनका उपभोग करता है। इस प्रकार पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रिया का ही नाम है।
पोषक के प्रकार
शरीर को ऊर्जा एवं पोषण देने वाला आहार में अनेक रासायनिक तत्त्वों का मिश्रण होता है। इन्हीं रासायनिक तत्वों को मनुष्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से 6 मुख्य समूहों में बाँटा गया है।
- प्रोटीन
- कार्बोज (कार्बोहाइड्रेट)
- वसा
- विटामिन्स
- खनिज लवण
- जल
कुपोषण
जब व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार भोजन ग्रहण नहीं करता, तब वह उस भोजन के पोषक तत्वों का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाता व उसका शारीरिक विकास उसकी आयु अनुसार नहीं होता और इससे उसकी कार्यक्षमता भी पूरी नहीं होती, तो वह कुपोषण कहलाता है।
भारतवर्ष में कुपोषण व उसके कारण
जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं मिलता या ऐसा भोजन मिलता हो जिसमें उसकी आवश्यकता से अधिक पोषक तत्त्व हों, तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की स्थिति को कुपोषण कहते हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा पोषण विज्ञान का हमारे देश की जनसंख्या को ज्ञान न होने के कारण हमारे देश में कुपोषण अधिक है और इसी कारण यहाँ मृत्यु-दर भी अधिक है। पोषक तत्त्वों के अभाव के कारण व्यक्ति अविकसित व रोगग्रस्त हो जाता है।
स्वास्थ्य की इस दशा के प्रमुख कारण निम्न हैं।
- खाद्य पदार्थों का अभाव
- निर्धनता
- अशिक्षा व अज्ञानता
- मिलावट
- जनसंख्या की अधिकता
कुपोषण के लक्षण
- शरीर – छोटा, अपर्याप्त रूप से विकसित
- भार – अपर्याप्त भार, आवश्यकता से अधिक या कम
- मांसपेशियाँ – छोटी या अविकसित, कम कार्यशील
- त्वचा तथा रंग-रूप – झुर्रिया युक्त,पीलापन लिए भूरे रंग की त्वचा
- नेत्र – अन्दर धंसी हुई निर्जीव आँखें ।
- निद्रा – निद्रा आने में कठिनाई
भोजन के कार्य
मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है, तब वह उस भोजन में निहित पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जब इन पौष्टिक तत्त्वों का सम्पादन शरीर में होता है, तो शरीर में इनका निम्न प्रभाव पड़ता है।
- शरीर का सुविकसित निर्माण।
- कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु ऊर्जा प्रदान करना।
- शरीर के प्रत्येक अंग को उसकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व पहुँचाकर क्रियाशील बनाए रखना।
- विभिन्न कार्यों को करते हुए या आयु अनुसार शरीर में हुई टूट-फूट की पूर्ति करना।
- शरीर में रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 1 पोषण एवं सन्तुलित आहार help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 1 पोषण एवं सन्तुलित आहार, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
![]()