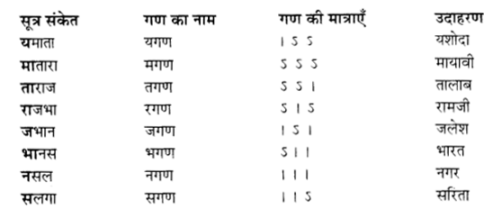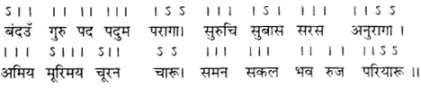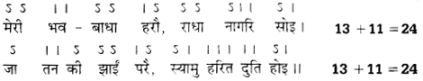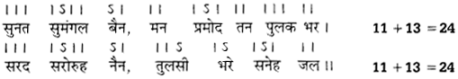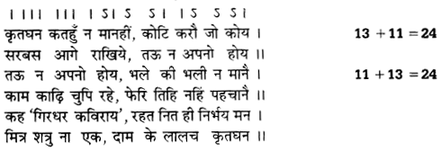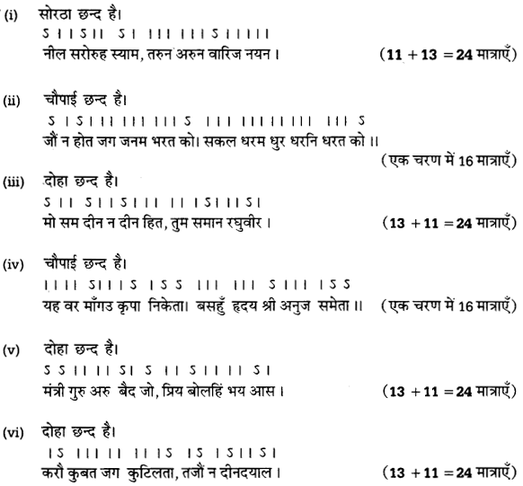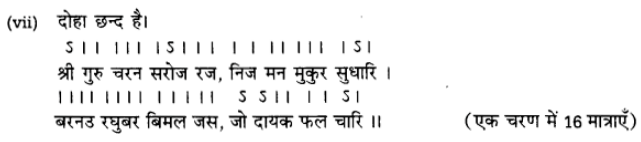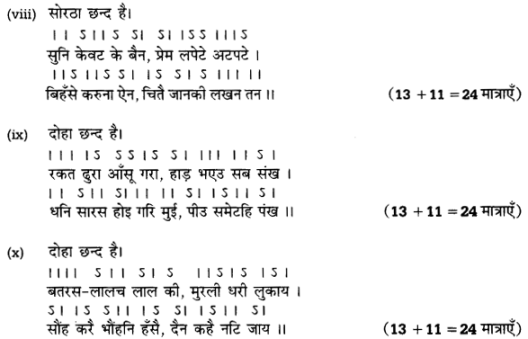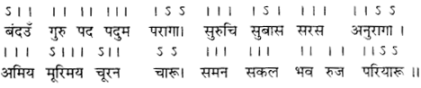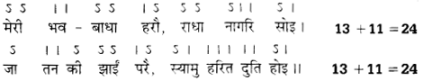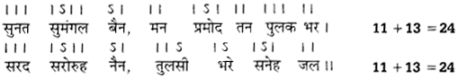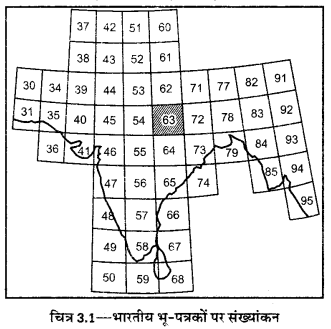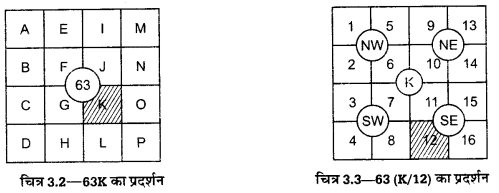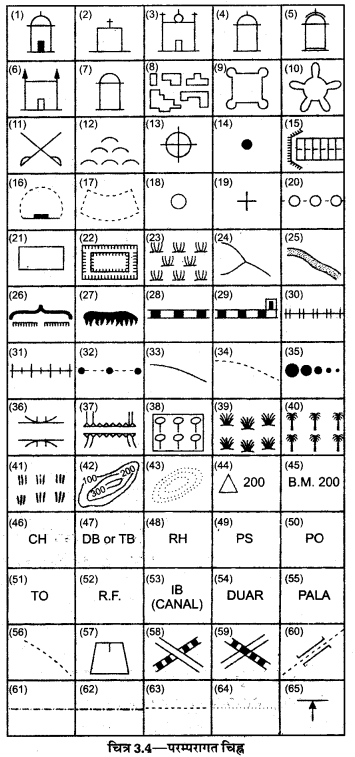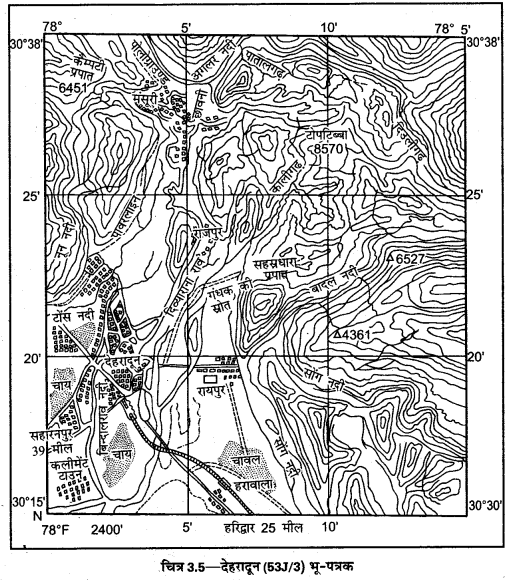UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त) are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त).
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Civics |
| Chapter |
Chapter 2 |
| Chapter Name |
Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त) |
| Number of Questions Solved |
21 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त)
विस्तृत उत्तीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1.
राज्य के आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों का वर्णन कीजिए। [2014, 16]
उत्तर
राज्य के कार्य
प्रत्येक युग के विचारकों का ध्यान राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्यक्षेत्र पर अवश्य गया है। सभी ने अपने समय की परिस्थितियों एवं ज्ञान के आधार पर राज्य के कार्यों का वर्णन किया है। देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार राज्य के कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। प्रारम्भिक समय में राज्य द्वारा केवल वे ही कार्य किए जाते थे, जिनको करना राज्य के अस्तित्व हेतु नितान्त आवश्यक था। लेकिन वर्तमान काल में राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। उसके कार्यों को एक सीमा में बाँधकर उनकी सूची तैयार करना असम्भव है। फिर भी राज्य द्वारा वर्तमान में जो कार्य किए जाते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-
(अ) राज्य के आवश्यक अथवा अनिवार्य कार्य तथा
(ब) राज्य के ऐच्छिक अथवा सामाजिक कार्य।
(अ) राज्य के आवश्यक अथवा अनिवार्य कार्य
अनिवार्य कार्यों का तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिनका सम्पादन करना प्रत्येक राज्य के लिए नितान्त आवश्यक है। इन कार्यों को रोकने से अथवा इन कार्यों के सम्पादन में असफल होने पर राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। राज्य के आवश्यक कार्य निम्नलिखित हैं-
1. बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना – देश की सुरक्षा करना प्रत्येक राज्य का अनिवार्य कार्य है। यदि राज्य इस कार्य को नहीं करे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य के लिए राज्य को जल, नभ तथा स्थल सेना रखनी पड़ती है। इसके साथ-साथ उसको अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना पड़ता है, जिससे आपातकाल | में आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहायता प्राप्त की जा सके।
2. आन्तरिक शक्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना – राज्य का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना, नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा, आन्तरिक उपद्रवों का दमन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। मैकाइवर के शब्दों में राज्य केवल शान्ति एवं व्यवस्था का प्रबन्ध ही नहीं करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह सर्वसाधारण की सुरक्षा एवं उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहयोग दे।” इसके लिए राज्य को अपराध निश्चित करने तथा दण्ड देने की व्यवस्था करनी पड़ती है।
3. न्याय का समुचित प्रबन्ध करना – देश में शान्ति की स्थापना पुलिस तथा सेना के बल पर ही नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए राज्य को कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड देने के लिए एक कुशल एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी करनी पड़ती है।
4. अधिकार तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना – नागरिक के अधिकार तथा कर्तव्यों की सीमा का निर्धारण करना और उन्हें विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सुविधाएँ प्रदान करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। वर्तमान लोकतन्त्रीय युग में नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यों का अत्यधिक महत्त्व है।
5. परिवार में कानूनी सम्बन्ध स्थापित करना – राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह कानून का निर्माण कर पारिवारिक जीवन को सुखी तथा सामुदायिक जीवन को सुसंगठित करे। अतः पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों के बीच कानूनी सम्बन्ध स्थापित करना भी उसका अनिवार्य कार्य है। इसके अन्तर्गत सम्पत्ति के क्रय-विक्रय और ऋण के लेन-देन इत्यादि के कानून सम्मिलित हैं।
6. मुद्रा की व्यवस्था करना – राज्य का एक आवश्यक कार्य मुद्रा की व्यवस्था करना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की मुद्रा-व्यवस्था पर विशेष रूप से आधारित होती है। मुद्रा के बिना राज्य का कार्य नहीं चल सकता। वर्तमान प्रत्येक देश में धन का अधिकांश लेन-देन बैंकों द्वारा किया जाता है और बैंकों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण है।
7. कर संग्रह करना – राज्य के कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता | होती है। धन के अभाव में राज्य एक क्षण भी नहीं चल सकता है। धन-प्राप्ति के लिए राज्य अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाता है। इस प्रकार कर लगाना और वसूल करना राज्य का एक अनिवार्य कार्य है।
(ब) राज्य के ऐच्छिक अथवा सामाजिक कार्य
राज्य के वे कार्य ऐच्छिक कहलाते हैं जिनको राज्य यदि सम्पादित न भी करे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, लेकिन व्यक्तियों के नैतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक कल्याण की वृद्धि हेतु ऐसे कार्य आवश्यक होते हैं। मानव जीवन को सुखी, सुन्दर एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए राज्य निम्नलिखित ऐच्छिक अथवा सामाजिक कार्य करता है-
1. शिक्षा की व्यवस्था – मानवीय व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास असम्भव है। अतः वर्तमान में शिक्षा का प्रबन्ध करना राज्य का महत्त्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। इसी कारण राज्य प्रारम्भिक शिक्षा का संचालन करते हैं। राज्यों द्वारा नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। नागरिकों की मानसिक चेतना के विकास के लिए राज्य पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं इत्यादि की स्थापना करता है।
2. सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध – सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुव्यवस्था, सफाई एवं चिकित्सा इत्यादि का प्रबन्ध राज्य ही करता है। संक्रामक रोग एवं महामारियों को रोकने के लिए राज्य कानून बनाता है तथा नगरों एवं ग्रामों की सफाई का प्रबन्ध करता है। राज्य नागरिकों की चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना करता है जहाँ नि:शुल्क अथवा उचित मूल्य पर चिकित्सा का प्रबन्ध रहता है।
3. सामाजिक सुधार – समाज सुधार हेतु प्रयास करना राज्य का एक नैतिक कर्तव्य है। प्रत्येक देश के सामाजिक जीवन में कुछ ऐसी कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ प्रचलित रहती हैं जो सामाजिक जीवन के विकास का मार्ग अवरुद्ध करती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कुछ समय पहले बालविवाह, छुआछूत, साम्प्रदायिकता इत्यादि का बोलबाला था लेकिन सरकार ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में कठोर प्रयास किए हैं। इसके फलस्वरूप बाल-विवाह एवं छुआछूत को समाप्त करने में तो भारत सरकार कुछ सीमा तक सफल रही है लेकिन साम्प्रदायिकता एवं जातीयता का जहर अभी तक समाज में व्याप्त है।
4. बेकारी का उल्मूलन – बेकारी चोरी, लूट तथा अन्य असामाजिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। अत: प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को रोजगार दे। इसके लिए राज्य नए कल-कारखानों एवं उद्योगों की स्थापना करता है।
5. निर्धन, वृद्ध एवं अपाहिजों की सुरक्षा – राज्य में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो वृद्ध, रोगी, अपाहिज अथवा असहाय होने के कारण स्वयं अपनी आजीविका नहीं कमा सकते। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की सहायता करे। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य निर्धन-गृह, अन्धाश्रम, मानसिक चिकित्सालय, अनाथालय इत्यादि का प्रबन्ध करता है। राज्यों द्वारा वृद्ध तथा असहायों को उनकी जीवन रक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
6. उद्योग-धन्धों का विकास – देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक उद्योग-धन्धों का विकास हो। इस बारे में राज्य का यह कर्तव्य है कि बड़े उद्योगों का वह स्वयं अधिग्रहण करके तथा छोटे एवं कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करे। इसके लिए राज्य को वित्तीय सहायता, औद्योगिक अन्वेषण केन्द्रों की सहायता तथा वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
7. कृषि का विकास-कृषि – प्रधान देशों की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कृषि का विकास ने हो। अतः राज्य को कृषि की उन्नति की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए सिंचाई का प्रबन्ध, श्रेष्ठ बीज, उत्तम खाद, कृषि सम्बन्धी नवीन तकनीक एवं उपकरणों की व्यवस्था तथा आपातकाल में किसानों की आर्थिक सहायता इत्यादि की व्यवस्था राज्य ही करता है।
8. श्रमिकों का कल्याण – श्रमिकों के हितों की रक्षा करना राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण न कर सके इसके लिए कारखाना कानून तथा श्रम कानूनों द्वारा सरकार पूँजीपतियों पर नियन्त्रण रखती है। काम के अधिकतम घण्टे, न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमिकों की दशा में सुधार तथा प्रबन्धक एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों के निष्पादन हेतु राज्य नियमों की रचना करता है।
9. यातायात एवं संचार – साधनों का विकास – यातायात तथा संचार-साधनों के अभाव में कोई भी देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य रेल, डाक एवं तार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि साधनों का अधिकतम विकास करता है।
10. ललित कला, साहित्य एवं विज्ञान को प्रोत्साहन – राष्ट्र के निर्माण में ललित कला, साहित्य एवं विज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक राज्य उन्हें प्रोत्साहित करता है।
11. मनोरंजन का प्रबन्ध – यह कहा जाता है कि श्रम के पश्चात् आराम एवं मनोरंजन जीवन को दीर्घायु बनाते हैं। मनोरंजन से जहाँ एक ओर शिथिल अंगों में स्फूर्ति का संचार होता है। वहीं दूसरी ओर शरीर को आवश्यक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः राज्य नागरिकों के मनोरंजन के लिए समुचित व्यवस्था करता है। वर्तमान में नागरिकों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु राज्य पार्क, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा, चिड़ियाघर, साहित्य परिषद् एवं खेल के मैदान इत्यादि की व्यवस्था करता है।
12. मादक पदार्थों पर नियन्त्रण – मादक पदार्थों, जैसे—शराब, गाँजा, भाँग, तम्बाकू, सिगरेट इत्यादि पर रोक लगाना भी राज्य का आवश्यक कर्तव्य हैं। जो राज्य इनकी उपेक्षा करते हैं, वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और राज्य पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। अतः राज्य को नागरिकों के कल्याणार्थ मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए।
13. राष्ट्रीय विकास योजनाओं का निर्माण – वर्तमान में राज्य का एक महत्त्वपूर्ण ऐच्छिक कार्य राष्ट्रीय विकास की योजनाओं का निर्माण करके उन्हें क्रियान्वित करना है।
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव जीवन की जटिलता बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप राज्य के कार्यों की सूची लम्बी तथा विशाल होती जा रही है। यहाँ महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य के ऐच्छिक तथा अनिवार्य कार्यों में अन्तर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। जो कार्य किसी राज्य द्वारा आज ऐच्छिक समझे जाते हैं वे ही कल अनिवार्य कार्यों की श्रेणी में भी आ सकते हैं। इस प्रकार राज्य के कार्यों का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
राज्य के कार्य-क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों को प्रतिपादन हो चुका है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के उचित कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत का अभाव है। प्राचीनकाल में व्यक्ति के हित और राज्य के हित को समान समझा जाता था। जॉन लॉक का मत था कि राज्य के कार्य-क्षेत्र की सीमाएँ व्यक्ति के प्राकृतिक और जन्मजात अधिकारों द्वारा निर्धारित होती हैं। इस मत के आधार पर यूरोप में हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त प्रचलित हुआ। हरबर्ट स्पेन्सर ने इस सिद्धान्त के आधार पर ही व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। यह कहा जाने लगा, “राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए।” कालान्तर में आदर्शवाद, अराजकतावाद, समाजवाद आदि विचारधाराएँ विकसित होकर राज्य के कार्य-क्षेत्र का निर्धारण अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुकूल करने लगीं। बीसवीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की भावना का विकास हुआ। इसने राज्य के कार्य-क्षेत्र का व्यापक विस्तार कर दिया।
भारतीय विचारकों ने पाश्चात्य विचारकों से बहुत पहले ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान किया था। मनु ने प्राचीनकाल में ही राज्य के कार्यों का निर्धारण कर दिया था। कालान्तर में कौटिल्य ने भी राज्य के कार्यों की सीमाओं का निश्चित किया था। लेकिन भारतीय विचारकों को दृष्टिकोण राजतन्त्रात्मक प्रणाली से प्रभावित था, जबकि आज विश्व के अधिकांश राज्यों में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापित है। यही कारण है कि इक्कीसवीं शताब्दी के इस प्रारम्भिक दौर में लोक-कल्याणकारी राज्य की श्रेष्ठता स्थापित हो चुकी है।

प्रश्न 2.
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [2014]
या
राज्य के कार्यों का व्यक्तिवादी सिद्धान्त क्या है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। [2007]
या
व्यक्तिवाद से आप क्या समझते हैं ? इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए।
या
“राज्य एक आवश्यक बुराई है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचारों के पक्ष में तीन तर्क दीजिए। [2007, 09]
या
व्यक्तिवाद की विशेषताएँ बतलाइए तथा समाजवाद से इसका अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2011, 2013]
या
“राज्य एक अनिवार्य बुराई है।” इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
व्यक्तिवादी सिद्धान्त
व्यक्तिवादी सिद्धान्त के समर्थक व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं। उनके अनुसार, राज्य के कार्य तथा कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करते हैं; अतः राज्यों के कार्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
इस सिद्धान्त के समर्थक एडम स्मिथ, जे०एस० मिल, हरबर्ट स्पेन्सर आदि थे। फ्रीमैन के शब्दों में, “सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है।’
एक अन्य लेखक के अनुसार, “राज्य एक अनिवार्य बुराई है।” अर्थात् यह एक ऐसी बुराई है। जिसे व्यक्ति विवश होकर अपनाता है; अतः इसे अधिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए।
बेन्थम के शब्दों में, “व्यक्ति के हित को समझे बिना समुदाय के हित की कल्पना करना कोरी बकवास है।”
व्यक्तिवादियों के अनुसार, “राज्य एक अयोग्य संस्था है।”
स्पेन्सर के शब्दों में, “विधानमण्डलों के अँगूठा टेक, अशिक्षित तथा अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत में अनेक भयंकर भूलें करके समाज को हानि पहुँचाई है। अतः भविष्य में उन पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
व्यक्तिवादी मत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र
व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक-से-अधिक सीमित कर दिया जाये। स्पेन्सर के मतानुसार, “व्यक्ति का स्थान समाज तथा राज्य के ऊपर होना चाहिए और राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जिन्हें व्यक्ति नहीं कर सकता। उनके अनुसार राज्य के केवल निम्नलिखित तीन कार्य होने चाहिए-
1. आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था करना – राज्य की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। राज्य में नागरिकों को घूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जुलने, आजीविका प्राप्त करने इत्यादि के अनेक अधिकार होते हैं, परन्तु समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे लोगों का जीवन व सम्पत्ति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे असामाजिक तत्वों का दमन कर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का प्रधान कर्तव्य है, इसीलिए राज्य पुलिस और सेना की सहायता से समाज में शान्ति और व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। राज्य अपराधों, उपद्रव, लूटमार, चोरी-डकैती, विद्रोह आदि को रोकता है।
2. देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना – कभी-कभी एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। आत्म-रक्षा प्रत्येक राज्य का प्रमुख कार्य होता है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने की दृष्टि से राज्य शक्तिशाली जल, थल तथा वायु सेना आदि रखता है। इस प्रकार बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना राज्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है।
3. न्याय और दण्ड की व्यवस्था करना – समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए न्याय की उत्तम व्यवस्था का होना भी अनिवार्य है। न्याय की समुचित व्यवस्था से ही दुर्बल और असहाय व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह पाएँगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसलिए न्याय का प्रबन्ध करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। न्याय के साथ दण्ड भी सम्बद्ध है। दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य अपराधी का सुधार होना चाहिए।
व्यक्तिवाद की विशेषताएँ
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- यह सिद्धान्त राज्य की सर्वव्यापक शक्ति का विरोध करता है।
- यह सिद्धान्त इस बात में विश्वास नहीं करता कि राज्य के अपने निजी व्यक्तित्व और अपने निजी उद्देश्य हैं। व्यक्ति स्वयं साध्य है और राज्य साधन।
- व्यक्तिवादी राज्य की निरंकुशता तथा असीमितता में विश्वास नहीं करते।
- यह सिद्धान्त ‘लैसिस फेयर’ (Laissez Faire) के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य को जो वह चाहे करने दो।
- व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य को मनुष्य के जीवन से अलग रहना चाहिए।
- व्यक्तिवादियों के मतानुसार, राज्य का कार्य मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, अपराधी को दण्ड देना और बाहरी शत्रु से देश की रक्षा करना है, अर्थात् राज्य का कार्य मनुष्य की रक्षा करना है न कि उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करना।
- व्यक्तिवादियों के अनुसार, राज्य का अस्तित्व मानव-स्वभाव की निर्बलता का कारण है।
- स्वतन्त्रता व्यक्तिवाद की आधारशिला है। यह सिद्धान्त राज्य को व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए केवल पुलिस संगठन का कार्य देना चाहता है। राज्य को ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो।
- व्यक्तिवादियों के अनुसार, “राज्य एक अभिशाप है, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छीनता है तथा एक ऐसी संस्था है जो बुरी होते हुए भी समाज से अराजकता और अव्यवस्था दूर करने के लिए आवश्यक है।
व्यक्तिवाद के पक्ष में तर्क (गुण)
व्यक्तिवादी सिद्धान्त के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-
1. नैतिक तर्क – व्यक्तिवाद के समर्थन में नैतिक तर्क यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व तथा विशेषता होती है। अत: यह आवश्यक है कि राज्य सभी व्यक्तियों को समान न समझे, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शिक्षा, व्यवसाय तथा मनोरंजन आदि कार्यों को करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मिल ने कहा है कि व्यक्तिगत जीवन में राजकीय हस्तक्षेप व्यक्ति के आत्म-विश्वास को नष्ट कर देता है, उसकी उत्तरदायित्व की भावना को कमजोर बनाता है तथा चारित्रिक विकास को अवरुद्ध कर देता
2. आर्थिक तर्क – एडम स्मिथ, माल्थस, मिल, रिकाड आदि अर्थशास्त्री इस विचारधारा के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति अपने हानि-लाभ तथा आर्थिक हितों को स्वयं ही भली प्रकार समझता है। अतः राज्य को व्यक्ति के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
3. ऐतिहासिक तर्क – व्यक्तिवादी अपने मत के समर्थन में ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप सदैव हानिकारक रहा है। राज्य ने मूल्य पर नियन्त्रण किया तो चोर-बाजारी बढ़ी, उत्पादन अपने हाथ में लिया तो भ्रष्टाचार बढ़ा और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप से क्रान्तियाँ हुईं। अतः राज्य को हस्तक्षेप न करने की नीति का ही पालन करना चाहिए।
4. प्राणिवैज्ञानिक तर्क – स्पेन्सर ने व्यक्तिवाद के समर्थन में नया तर्क प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, यह प्राकृतिक नियम है कि सभी प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष में योग्य तथा सबल प्राणी ही जीवित रहते हैं तथा शेष नष्ट हो जाते हैं। अयोग्य और निर्बल व्यक्तियों के नष्ट होने से एक उन्नत और शक्तिशाली राज्य का निर्माण सम्भव होता है। स्पेन्सर ने यहाँ तक कहा कि राज्य को निर्धन, अपाहिज व अनाथों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जैविक नियमों के विरुद्ध है। राज्य को अपनी ऊर्जा योग्य व्यक्तियों के विकास के लिए लगानी चाहिए, क्योंकि वे ही समाज में रन के रूप में होते हैं।”
5. व्यावहारिक तर्क – व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि व्यावहारिक दृष्टि से : राज्य में सभी कार्यों को सम्पन्न करने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि राज्य के कर्मचारी लगन और प्रतिबद्धता से कार्य नहीं करते और मन्त्री प्रायः अनुभवशून्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समस्याएँ स्थानीय प्रकृति की होती हैं तथा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें देरी किये बिना सम्पन्न करना आवश्यक होता है। इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर जितनी जल्दी निपटाया जा सकता है, सरकारी स्तर पर उतना शीघ्र नहीं।
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना (दोष)
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है-
1. व्यक्ति और समाज की गलत कल्पना – वास्तविकता यह है कि “मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। समाज से उसका अटूट सम्बन्ध है। समाज तथा राज्य के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी विचारधारा गलत धारणा पर आधारित है।
2. स्वतन्त्रता का भ्रामक अर्थ – वस्तुतः राज्य अपने कानूनों द्वारा स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता, अपितु उसकी रक्षा करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादियों की स्वतन्त्रता विषयक धारणा गलत मान्यताओं पर टिकी है।
3. राज्य को अनिवार्य बुराई कहना गलत – अरस्तू ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की रक्षा के लिए हुई है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए ही वह स्थिर है। अतः राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं, अपितु एक सकारात्मक अच्छाई है।
4. राज्य मानव की उन्नति में बाधक नहीं – राज्य मनुष्यों की सर्वांगीण उन्नति के लिए। समुचित अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान करता है। मानव-समाज ने राज्य की छत्रछाया में ही पर्याप्त आर्थिक व वैज्ञानिक उन्नति की है। इसलिए राज्य मानव-उन्नति में बाधक नहीं है। अरस्तु के अनुसार, “राज्य समस्त विज्ञानों, समस्त कलाओं, समस्त गुणों तथा समस्त पूर्णता में सहायक है।”
5. राज्य को हस्तक्षेप आवश्यक – राज्य के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। उसका ऐसा प्रयत्न दूसरे व्यक्ति के ऐसे ही प्रयत्नों में बाधक हो सकता है जो परस्पर संघर्ष को जन्म देगा। इसलिए व्यक्तिवादियों का यह मत गलत है कि राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक है।
6. लोकतन्त्रीय युग में व्यक्तिवाद अनावश्यक – व्यक्तिवाद का जन्म निरंकुश राज्यों की प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ था। वर्तमान युग में लोकतन्त्र के उदय तथा लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा के उद्भव से ऐसी परिस्थिति नहीं है; अतः आज यह सिद्धान्त अमान्य है।
7. व्यक्तिवादी तर्क अमानवीय – लीकॉक ने कहा है कि “यदि शक्ति को ही जीवित रहने की कसौटी मान लिया जाए तो एक समृद्ध और सबल चोर समाज में प्रशंसा का पात्र होगा और एक भूखा कलाकार घृणा का।” इस प्रकार शारीरिक शक्ति बौद्धिक बल पर हावी हो जाएगी, जिसे जंगल-राज कह सकते हैं; अतः व्यक्तिवादी सिद्धान्त अमानवीय है।
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यक्तिवादी सिद्धान्त वर्तमान समय में प्रभावहीन हो गया है, तथापि इस सिद्धान्त का महत्त्व इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि राज्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना चाहिए। वस्तुतः व्यक्तिवाद व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतन्त्रता पर बल देती है। गार्नर के शब्दों में, “व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के महत्त्व को विश्व के समक्ष रखा है।”
व्यक्तिवाद और समाजवाद में अन्तर
1. विचारधारा – व्यक्तिवादी सिद्धान्त के समर्थक व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। उनके अनुसार, राज्य के कार्य तथा कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करते हैं; अत: राज्य के कार्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। वे राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। । दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किये जाने चाहिए जो व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हों। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के कार्यों की कोई सीमा नहीं है तथा सामाजिक जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं।
2. कार्यक्षेत्र – व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक-से-अधिक सीमित कर दिया जाए। स्पेन्सर के मतानुसार, “व्यक्ति का स्थान समाज तथा राज्य के ऊपर होना चाहिए। और राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जिन्हें व्यक्ति नहीं कर सकता।” उनके अनुसार राज्य के केवल तीन निम्नलिखित कार्य होने चाहिए-
- आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था करना,
- देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना तथा
- न्याय और दण्ड की व्यवस्था करना।
दूसरी ओर समाजवादी समानता को अपना आदर्श मानकर चलते हैं और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अधिकाधिक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष बल देते हैं-
- समाज की आंगिक एकता,
- समाज में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग,
- पूँजीवाद का अन्त तथा
- उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व।
उद्योगों के प्रति दृष्टिकोण
व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के कार्यों को न्यूनतम कर देना चाहती है तथा उद्योगों को व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से खुला रखना चाहती है। वह उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा विकासे में राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहती। वह खुली प्रतियोगिता में विश्वास रखती है तथा एक प्रकार से पूँजीवाद की समर्थक है।
दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा पूँजीवाद की घोर विरोधी होने के कारण भूमि और उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्त की माँग करती है। यह विचारधारा उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहती है। समाजवादी विचारधारा के अनुसार वैयक्तिक उद्योग वैयक्तिक लूटमार है और व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामाजिक अथवा सामूहिक सम्पत्ति का रूप देना ही उचित है।
अतः निष्कर्षतया कहा जा सकता है कि उद्योगों के निजीकरण की प्रवृत्ति समाजवादी विचारधारा के प्रतिकूल है।
प्रश्न 3.
लोक-कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह समाजवादी राज्य से किस प्रकार भिन्न है? [2010]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। [2010, 12, 16]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दीजिए। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? [2011, 15]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य का अर्थ है? इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। [2008]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना में कहाँ तक सफलता मिली है?
या
कल्याणकारी राज्य के कार्यों का उल्लेख विस्तार से कीजिए। [2013, 14]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताइए तथा इसके तीन महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। [2013]
या
लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है ? इसके मुख्य उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। [2008, 12, 13]
उत्तर
लोक-कल्याणकारी राज्य
लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा वर्तमान युग की देन है। सामान्य शब्दों में, लोककल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के विकास व उसकी उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है।
विभिन्न विद्वानों द्वारा लोक-कल्याणकारी राज्य का अर्थ विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नवत् हैं-
- केण्ट के अनुसार, “लोक-कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज-सेवाओं की व्यवस्था करता है।
- पण्डित नेहरू के शब्दों में, “सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, अमीरों व गरीबों के बीच का अन्तर मिटाना, जीवन-स्तर को ऊपर उठाना, लोक-कल्याणकारी राज्य के आधारभूत – ‘तत्त्व हैं।”
- अब्राहम लिंकन के अनुसार, “कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान उद्देश्य के वितरण से करता है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि “जो राज्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में जनता के कल्याण के लिए अधिक-से-अधिक कार्य करता है, उसे लोक-कल्याणकारी राज्य कहते हैं। एक लोक-कल्याणकारी राज्य नागरिकों की स्वतन्त्रता और समानता का पोषक होता है। वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समानता के बीच सन्तुलन बनाये रखने में सहायक होता है तथा पारस्परिक सहयोग को महत्त्व प्रदान करता है।”
लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्षण या विशेषताएँ या उद्देश्य
लोक-कल्याणकारी राज्य की उपर्युक्त धारणा को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के राज्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं-
1. आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था – लोक-कल्याणकारी राज्ये प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथों में केन्द्रित होती है, जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। लोक-कल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य निम्नलिखित तीन बातों से लिया जा सकता है-
(i) सभी व्यक्तियों को रोजगार – ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उनकी योग्यतानुसार उन्हें किसीन-किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सका है, उनके जीवनयापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगार बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(ii) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी – एक व्यक्ति को अपने कार्य के बदले में इतना पारिश्रमिक अवश्य ही मिलना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति की जा सके। न्यूनतम जीवन-स्तर से आशय है-भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ। लोक-कल्याणकारी राज्य में किसी एक के लिए अधिकता के पूर्व सबके लिए पर्याप्तता की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(iii) अधिकतम समानता की स्थापना – सम्पत्ति और आय की पूर्ण समानता न तो सम्भव है और न ही वांछनीय; तथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात् होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा सम्बन्धी कार्य से उचित अनुपात होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके।
2. राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था – लोक-कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और ये अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-
(i) लोकतन्त्रीय शासन-लोक – कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही आवश्यक समझा जाता है; अतः एक लोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था वाला राज्य ही लोक-कल्याणकारी राज्य हो सकता है।
(ii) नागरिक स्वतन्त्रताएँ – संविधान द्वारा लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना कर देने से ही राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतन्त्रता का वातावरण होना चाहिए, अर्थात् नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती और लोकहित की साधना के बिना लोक-कल्याणकारी राज्य, आत्मा के बिना शरीर के समान होगा।
पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन आदि साम्यवादी राज्यों में नागरिकों के लिए नागरिक स्वतन्त्रताओं और परिणामतः राजनीतिक सुरक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता।
3. सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था – सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है। और इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और सम्पत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अन्त करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्त्व प्रदान किया जाए। डॉ० बेनी प्रसाद के शब्दों में, “सामाजिक समानता का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्त्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधनमात्र नहीं समझा जा सकता है। वस्तुत: लोक-कल्याणकारी राज्य में जीवन के सभी पक्षों में समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।
4. राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि – लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए, जिनके करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट या कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था वरन् जैसा कि हॉब्सन ने कहा है, “डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कम्पनी के एजेण्ट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियन्त्रक तथा अन्य सैकड़ों रूपों में कार्य किया जाना चाहिए।”
5. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना – इन सबके अतिरिक्त एक लोक-कल्याणकारी राज्य, अपने राज्य विशेष के हितों से ही सम्बन्ध न रखकर सम्पूर्ण मानवता के हितों से सम्बन्ध रखता है और इसका स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होता है। एक लोक-कल्याणकारी राज्य तो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् ‘सम्पूर्ण विश्व ही मेरा कुटुम्ब है’ के विचार पर आधारित होता है।
लोक-कल्याणकारी राज्य के कार्य
परम्परागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों (अनिवार्य और ऐच्छिक) में विभाजित करने की रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए किये जाने जरूरी हैं, किन्तु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की. विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणामस्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की यह सीमा रेखा समाप्त हो गयी है और यह माना जाने लगा है। कि परम्परागत रूप में ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
1. आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था करना – राज्य की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। राज्य में नागरिकों को घूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जुलने, आजीविका प्राप्त करने इत्यादि के अनेक अधिकार होते हैं, परन्तु समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे लोगों का जीवन में सम्पत्ति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे असामाजिक तत्वों का दमन कर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का प्रधान कर्त्तव्य है, इसीलिए राज्य पुलिस और सेना की सहायता से समाज में शान्ति और व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। राज्य अपराधों, उपद्रव, लूटमार, चोरी-डकैती, विद्रोह आदि को रोकता है।
2. देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना – कभी-कभी एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। आत्म-रक्षा प्रत्येक राज्य का प्रमुख कार्य होता है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने की दृष्टि से राज्य शक्तिशाली जल, थल तथा वायु सेना आदि रखता है। इस प्रकार बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना राज्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है।
3. न्याय और दण्ड की व्यवस्था करना – समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए। न्याय की उत्तम व्यवस्था का होना भी अनिवार्य है। न्याय की समुचित व्यवस्था से ही दुर्बल और असहाय व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह पाएँगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसलिए न्याय का प्रबन्ध करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। न्याय के साथ दण्ड भी सम्बद्ध है। दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य अपराधी का सुधार होना चाहिए।
4. वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन – आज के युग में प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करता है। वह दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजता है और दूसरे देशों के राजदूतों को अपने देश में रखता है। आपसी झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करता है। दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समझौते करके राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इस कार्य का महत्त्व आजकल इतना अधिक हो गया है कि प्रत्येक राज्य में इसके लिए एक पृथक् विभाग की स्थापना हो गयी है।
5. मुद्रा का प्रबन्ध करना – गैटिल तथा कुछ अन्य विचारकों ने राज्य के आवश्यक कार्यों के अन्तर्गत मुद्रा प्रबन्ध को भी स्थान दिया है। वास्तव में मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, है। मुद्रा के द्वारा ही राज्य अपनी आर्थिक नीति को सुनियोजित करता है। मुद्रा के द्वारा ही आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है; अतः राज्य उचित व प्रगतिशील मुद्रा-प्रणाली की व्यवस्था करता है।
6. कर लगाना.एवं वसूल करना – राज्य की आय के अनेक स्रोत होते हैं। इन स्रोतों में कर संग्रह प्रमुख है। राज्य करों की रूपरेखा, उनका अनुपात तथा दरें निश्चित करता है। वह निर्धारित करता है कि किससे कितना कर लेना चाहिए। कर-निर्धारण तथा कर (संग्रह) का सम्पादन किन लोगों द्वारा किस रूप में होना चाहिए, यह कार्य भी राज्य द्वारा निश्चित किया जाता है।
7. शिक्षा का प्रबन्ध करना – शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होती है। शिक्षा की इस महत्ता के कारण सभी सभ्य राज्य शिक्षा, विकास तथा संगठन का प्रयास करते हैं। इस कार्य की पूर्ति के लिए राज्य विद्यालय, प्रयोगशाला, शोधशाला, वाचनालय, संग्रहालय इत्यादि की व्यवस्था करता है। इसके लिए राज्य स्वतः शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करता है, उनका संचालन करता है तथा राज्य के नागरिकों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देता है।
8. स्वास्थ्य-रक्षा एवं सफाई का प्रबन्ध करना – राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए उसके नागरिकों को स्वस्थ होना परम आवश्यक है। जिस राज्य के नागरिक स्वस्थ नहीं होते, उस राज्य का विकास नहीं हो पाता। अतः राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सफाई की ओर पूरा ध्यान देता है। यह बीमारियों की रोकथाम करता है, खाद्य-पदार्थों में मिलावट को रोकता है। एवं हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाता है। एक अच्छे राज्य का यह कर्तव्य है। कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर पूरा ध्यान दे। अच्छे चिकित्सालयों की स्थापना करे, जहाँ नि:शुल्क उपचार और चिकित्सा की व्यवस्था हो।
9. सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना – प्राय: प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित होती हैं। ये समाज के स्वरूप को विकृत कर देती हैं। इनके कारण सामाजिक प्रगति में बाधा पहुँचती है। राज्य को इन कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए। स्वाधीन भारत की सरकार ने भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों; जैसे-बाल-विवाह, सती–प्रथा, दहेज-प्रथा, छुआछूत आदि को कानून द्वारा दूर करने का अच्छा प्रयास किया है।
10. उद्योग-धन्धों तथा व्यापार का विकास करना – राज्य के ऐच्छिक कार्यों में उद्योग-धन्धों तथा व्यापार का विकास भी सम्मिलित है। वास्तव में किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के द्वारा ही समाज की चहुंमुखी प्रगति हो सकती है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह उद्योग-धन्धों तथा व्यापार का समुचित विकास करे, जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते करना, व्यापारियों तथा उत्पादकों को आर्थिक सहायता देना, कुछ उद्योगों को स्वयं चलाना, अधिक आयात कर लगाना आदि अनेक उपाय राज्य को अपनाने चाहिए।
11. यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करना – यातायात एवं संचार के साधन किसी राष्ट्र की शिराओं या धमनियों की भाँति होते हैं। समुचित आवागमन एवं संचार के साधनों के बिना कोई राष्ट्र अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक राज्य रेल, तार, डाक, वायुयान, नौका-परिवहन इत्यादि का विकास करता है। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने विगत वर्षों में इस दिशा में स्तुत्य कार्य किये हैं। इन साधनों के विकास से आर्थिक उन्नति तथा राष्ट्रीय प्रगति को बड़ा सम्बल मिला है।
12. बेकारी का अन्त करना – प्रायः प्रत्येक समाज में बेरोजगार लोग होते हैं। एक उन्नत और सभ्य राज्य बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रयास करता है। इसलिए वह नये उद्योगधन्धों एवं आजीविका के नये स्रोतों की स्थापना करने का प्रयास करता है। कुछ राज्य बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं।
13. कृषि और ग्रामों का विकास करना – प्रायः प्रत्येक राष्ट्र में किसी-न-किसी सीमा तक कृषि-कार्य किया जाता है। कृषि के उत्पादन पर ही बहुत कुछ राष्ट्र की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवलम्बित होती है। अतएव प्रत्येक राज्य कृषि के विकास का पूरा प्रयास करता है। इस कार्य के लिए राज्य सिंचाई के साधनों का विकास, अच्छे बीज, खाद तथा आधुनिक कृषि-यन्त्रों की व्यवस्था करता है तथा फसल की रक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। साथ ही कृषि-उपजों की उचित मूल्य पर खरीद भी करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामों में सुधार और कृषकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना भी राज्य का कार्य है।
14. मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना – मनोरंजन को मनुष्य के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना स्वस्थ और सफल जीवन सम्भव नहीं है। इसलिए राज्य मनोरंजन के स्वस्थ साधनों का प्रबन्ध करता है। वह पार्क-बगीचे, खेल-कूद के मैदान, रेडियो, दूरदर्शन, नाट्य-गृह आदि की व्यवस्था करता है। लेकिन राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन के साधनों में अश्लीलता का प्रवेश न होने पाये।
15. श्रमिकों के हितों की रक्षा करना – आज का युगे औद्योगिक युग है। ऐसे युग में औद्योगिक संस्थानों में काम करने वालों की संख्या काफी है। प्रायः पूँजीपति अनेक प्रकार से श्रमिकों का शोषण करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रगतिशील राज्य श्रमिकों के काम के घण्टे, उनकी छुट्टियाँ, वेतन-भत्ता, अवकाश इत्यादि से सम्बन्धित श्रम कानूनों का निर्माण करता है, जिनके द्वारा श्रमिक मिल-मालिकों के अत्याचारों तथा शोषण से बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य श्रमिकों के मनोरंजन का प्रबन्ध करता है और उनके हितों की हर सम्भव दृष्टि से सुरक्षा करता है।
16. कला, साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति में सहयोग करना – किसी भी राष्ट्र की प्रगति । उसकी कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति पर ही निर्भर करती है। अतः प्रत्येक राज्य को यह परम कर्तव्य है कि वह देश की विविध कलाओं, सभी भाषाओं के साहित्य और विज्ञान की उन्नति में सहयोग प्रदान करे, जिससे कलाकार, साहित्यकार और वैज्ञानिक प्रोत्साहित होकर देश के विकास में अपना अधिकाधिक योगदान दे सकें।
17. सामाजिक कल्याण के अन्य कार्य करना – उपर्युक्त ऐच्छिक कार्यों के अतिरिक्त कतिपय राज्य अन्य प्रकार के सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। वे महिलाओं के कल्याण, शिशुओं के कल्याण, अपाहिजों के कल्याण, वृद्धों के कल्याण इत्यादि के लिए कानून का निर्माण कर उनको आवश्यक सुविधाएँ देने का प्रयास करते हैं। अनेक राज्यों में अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, रोजगार में वरीयता तथा वृद्धों को पेंशन देने की व्यवस्था होती है। भारत सरकार ने भी सामाजिक कल्याण को निश्चित गति तथा दिशा देने का प्रयास किया है।
निष्कर्ष-राज्य के उपर्युक्त कार्यों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। आज के युग में राज्य के कार्यों की सीमा में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन आ गया है। सभ्यता के विकास के साथ ही राज्य के कार्यों में भी वृद्धि होती जा रही है। वास्तव में, राज्य का उद्देश्य सारे समाज का कल्याण करना होना चाहिए।
क्या भारत कल्याणकारी राज्य है ?
भारत में प्राचीन काल से ही कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अपनाया जाता रहा है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ ‘अर्थशास्त्र में इस आदर्श का दृढ़ समर्थन किया था। चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट् अशोक, शेरशाह सूरी तथा अकबर आदि सभी प्रजा के कल्याण को प्रमुखता देते रहे।
1947 ई० में स्वतन्त्र होने के बाद भारत के संविधान-निर्माताओं ने संविधान में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया और कल्याणकारी राज्य के सभी प्रमुख तत्त्वों को संविधान में स्थान दिया। संविधान की अग्रलिखित विशेषताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है-
- संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतन्त्रता तथा समानता प्रदान की गयी है।
- संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख करके नागरिकों को सर्वांगीण उन्नति में समान अवसर प्रदान किये गये और संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उल्लेख तो एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य के तत्वों की घोषणा-पत्र है।
- पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में जन-कल्याण व विकास के अनेक कार्य सम्पन्न हुए हैं।
- आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। गरीबी व बेकारी दूर करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।
- शिक्षा, समाज-कल्याण व स्वास्थ्य-सुधार के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किये गये हैं।
व्यक्तिवादियों के अनुसार, “व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन।” लोक-कल्याणकारी राज्य को सर्वमान्य लक्ष्य आर्थिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति होता है। इस दृष्टि से वर्ष 1971-76 के काल में लोक-कल्याण की दिशा में राजाओं के प्रिवीपर्स की समाप्ति, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, शहरी सम्पत्ति का समीकरण आदि कदम उठाये गये। वस्तुत: आर्थिक सुरक्षा तथा समानता की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वास्तविक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना से भारत अभी भी बहुत दूर है। इस सम्बन्ध में तीव्र गति से ठोस प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।
कल्याणकारी राज्य व समाजवादी राज्य में भिन्नता
समाजवाद एवं लोक-कल्याणकारी राज्यों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो अन्तर हैं-
- लोक-कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी एवं अधिकतम आर्थिक समानता से है।
समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है यद्यपि समानता का यह विचार प्राकृतिक विधान और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। समाजवाद का आर्थिक समानता का विचार पूँजीवाद के अन्त में निहित है।
- समाजवाद राज्य को अधिकाधिक कार्य सौंपना चाहता है। समाजवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। इसके विपरीत कल्याणकारी राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य सौंपना चाहते हैं जिनके करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होती। लोक-कल्याणकारी राज्य नागरिक स्वतन्त्रताओं के हिमायती हैं।

प्रश्न 4.
मनु का राजत्व सिद्धान्त क्या था? उसके अनुसार राज्य के किन्हीं चार कार्यों की विवेचना कीजिए। [2009, 10]
या
मनु और कौटिल्य की राज्य के प्रति क्या अवधारणा थी? तर्कसंगत विवेचना कीजिए। [2012]
या
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में मनु के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। [2011]
या
राज्य के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित मनु के विचार लिखिए। मनु के अनुसार राजा निरंकुश क्यों नहीं हो सकता है? [2013]
उत्तर
प्राचीन विचारकों- मनु, शुक्र, बृहस्पति और कौटिल्य आदि ने राज्य के कार्यों और राजा के कर्तव्यों पर विस्तार से विचार किया है। सामान्य रूप से उन्होंने प्राचीन भारत के राजनीतिक चिन्तन में राज्य को व्यापक कार्यक्षेत्र प्रदान किया है।
मनु का राजत्व सिद्धान्त
राज्य के कार्यक्षेत्र और राजा की शक्तियों के प्रसंग में आचार्य मनु के राजनीतिक चिन्तन की निम्नलिखित दो बातें प्रमुख हैं-
(क) मनु ने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि राजा द्वारा कर्तव्यपालन किया जाना चाहिए और राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है—प्रजा-पालन। मनु के शब्दों में, “राजा को अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का श्रेष्ठ धर्म है और प्रजा-पालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म से युक्त होता है।”
(ख) उसने राजा को निरंकुश शक्तियाँ प्रदान नहीं कीं, वरन् राजसत्ता को सीमित किया है। मनु के अनुसार, राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता, धर्म राजाओं और जनसाधारण पर एकसमान ही शासन करता है। इसके अतिरिक्त, राजा (राजनीतिक प्रभु) जनता के भी अधीन है। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग करने में जनता की आज्ञा-पालन की क्षमता से सीमित होता है। सालेटोर के अनुसार, “मनु ने निस्सन्देह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है।”
राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में मनु के चिन्तन की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसने मानवमात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म-पालन पर बल दिया है जिसे अपनाकर सम्पूर्ण मानव-जाति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। मनु ने ऐसी कानूनी पद्धति तथा राजधर्म का वर्णन किया है। जिसमें सभी वर्गों के व्यक्तियों के कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है।
मनु के अनुसार राज्य के कार्य
मनु ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘मनुस्मृति’ में राज्य के कार्यों पर समुचित विचार किया है। मनु के अनुसार, राज्य के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य हैं-
1. बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना – मनु के मत से राज्य का सर्वप्रमुख कार्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। मनु के अनुसार, राजा को चाहिए कि वह सेना को तैयार रखे, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहे और अपने गुप्तचरों की सहायता से शत्रु की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करे। उसे अप्राप्त को पाने की इच्छा और प्राप्त भूमि की रक्षा करनी चाहिए। राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए, क्योंकि वह सभी दुर्गों में श्रेष्ठ होता है।
2. आन्तरिक शान्ति स्थापित करना – मनु यह मानते थे कि समाज के अराजक तत्त्व आन्तरिक शान्ति भंग करने का कारण बन सकते हैं, इसलिए राज्य का एक प्रमुख कार्य दण्ड-शक्ति के आधार पर दुष्टों को नियन्त्रण में रखना है। राज्य के द्वारा उनके प्रति बहुत कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए। राज्य को भ्रष्ट व्यक्तियों, जुआरियों तथा धोखेबाजों को दण्डित करना चाहिए और गलत ढंग से चिकित्सा करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार, वैश्यों और शूद्रों को अपने कर्तव्यों का सुचारु रूप से पालन करने के लिए विवश करना भी राज्य का कार्य है। मनु इस बात पर भी बल देता है कि स्त्रियों की सम्पत्ति को हथियाने वाले व्यक्तियों को राज्य द्वारा कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।
3. विवादों का निर्णय (न्यायिक कार्य) करना – राज्य का एक प्रमुख कार्य लोगों के आपसी विवादों का निर्णय करना और विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा करना है। इस हेतु न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए ताकि जनसाधारण को निष्पक्ष न्याय सुलभ हो सके। राज्य को इन सभी विवादों का निर्णय धर्म-विधानों का ध्यान रखकर करना चाहिए। मनु के अनुसार, “जिस सभा (न्यायालय) में असत्य द्वारा सत्य पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं।”
4. राज्य का आर्थिक विकास और प्रगति करना – मनु राज्य का अन्य प्रमुख कार्य राज्य का आर्थिक विकास और प्रगति बताते हैं। मनु के अनुसार, “राजा अप्राप्त (न मिले हुए सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात, भूमि आदि) को दण्ड द्वारा (शत्रु को दण्ड देकर या जीतकर) पाने की इच्छा करे। प्राप्त (मिले हुए सोना आदि) द्रव्यों की देखभाल करते हुए रक्षा करे तथा रक्षित धन की वृद्धि करे और बढ़ाये गये (उन द्रव्यों) को सुपात्रों में दान कर दे।” (मनुस्मृति, 7:101)
इस प्रकार शासन की नीति चार सूत्री होनी चाहिए-
- शक्ति और वैध उपायों द्वारा धन अर्जित करना,
- धन का रक्षण करना,
- धन में वृद्धि करना,
- धन सुपात्रों को दान करना।
कर की व्यवस्था (Taxation) करना – राज्य में सभी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए मनु ने अनेक करों (Taxes) का सुझाव दिया है। मनु ने निम्नलिखित चार प्रकार के कर बताये है-
- बलि-विभिन्न प्रकार के कर।
- शुल्क–बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री के लिए लायी गयी वस्तुओं पर चूँगी।
- दण्ड-कर-जुर्माने।
- भाग-लगान।
मनु द्वारा निर्दिष्ट कर-सम्बन्धी धारणा में उसकी बुद्धिमत्ता और लोक-कल्याणकारी प्रवृत्ति की झलक मिलती है। मनु राज्य की प्रगति के लिए राज्य द्वारा कर लिया जाना आवश्यक मानते हैं, किन्तु वे कर को उचित सीमा तक ही लिये जाने का समर्थन करते हैं। मनु के अनुसार, “कर न लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अन्त हो जाता है।” अधिक कर का निषेध करते हुए मनु कहते हैं- जिस प्रकार बछड़ा और मधुमक्खी अपने खाद्य क्रमशः दुध और मधु थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राज्य को प्रजा से। थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। मनु का मत था कि कर इस प्रकार निर्धारित हो कि निर्धन जनता पर कर का बोझ कम पड़े और समृद्ध व्यक्ति अधिक कर का भार उठाये। मनु ने वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण रखने को राज्य का एक कर्तव्य माना।
5. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्रबन्ध करना – मनु राज्य द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्रबन्ध किये जाने का समर्थन करता है। उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण माना है और स्थानीय विषयों का भार इन संस्थाओं को ही सौंपने का निर्देश दिया है।
6. असहाय व्यक्तियों की सहायता करना – मनु असहाय व्यक्तियों की सहायता करना भी राज्य का प्रमुख कार्य मानता है। उसके अनुसार, राज्य द्वारा सन्तानविहीन स्त्रियों, विधवाओं तथा रोगियों की देखभाल की जानी चाहिए और अवयस्कों की सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।
7. शिक्षा का प्रबन्ध करना – राज्य को शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए तथा उसे शिक्षकों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राज्य के द्वारा वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने वाले ब्राह्मणों को दान देकर आर्थिक सहायता की जानी चाहिए।
इस प्रकार मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत व्यापक माना है, किन्तु उसे निरंकुश नहीं बताया है। राजा धर्म के अधीन है। वह धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। केवल मोटवानी का मत है, “मनु के निर्देशन में राज्य द्वारा बनाये जाने वाले अनेक कानून वर्तमानकालीन राजशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होंगे।”
वस्तुतः मनु द्वारा व्यक्त राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
कौटिल्य की राज्य के प्रति अवधारणा तथा राज्य सम्बन्धी सप्तांग सिद्धान्त
कौटिल्य के अनुसार, राजा के द्वारा उपर्युक्त सभी कार्यों को सम्पादन लोकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए।
कौटिल्य राजतन्त्र को शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है। वह राज्य के सात अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। इतना होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। उस पर निम्नलिखित कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता-.
1. अनुबन्धवाद – कौटिल्य के अनुसार, मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की उसके बदले में राजा ने अपनी प्रजा के धन-जन की रक्षा का वचन दिया था। इसीलिए राजा प्रजा के जन-धन को हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकता। कौटिल्य का मत है कि राजा की स्थिति वेतन-भोगी सैनिकों के समान ही होती है, अर्थात् राजा राजकोष से निश्चित वेतन ले सकता है। उसे मनमाने ढंग से राज्य की सम्पत्ति को व्यय करने का अधिकार नहीं था।
2. धर्म और रीति-रिवाज – कौटिल्य के अनुसार, राजा के अधिकार धर्म और रीति-रिवाज सीमित थे और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य था। उसे यह डर रहता था कि राजा द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जनता क्षुब्ध होकर स्वयं ही उसके जीवन का अन्त न कर दे। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक को भये भी राजा को मनमानी करने से रोकता था।
3. मन्त्रिपरिषद् – राजा की शक्ति पर मन्त्रिपरिषद् का भी प्रतिबन्ध होता था। उसके अनुसार राजा और मन्त्रिपरिषद् राज्य रूपी रथ के दो चक्र हैं, इसीलिए मन्त्रिपरिषद् का अधिकार राजा के बराबर ही है। मन्त्रिपरिषद् राजा की शक्ति पर नियन्त्रण रख उसे मनमानी करने से रोकती थी।
4. राजा का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षा – राजा का व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गयी शिक्षा भी कौटिल्य के राजा की निरंकुशता पर अत्यन्त प्रभावशाली प्रतिबन्ध है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक गुण आवश्यक बताये हैं और ऐसा सर्वगुणसम्पन्न राजा अपने स्वभाव से निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहे हैं कि वह लोकहित के कार्यों में लगा रहे। श्री कृष्णराव ने ठीक ही कहा है कि “कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है।”
प्रश्न 5.
राज्य के कार्यों से सम्बन्धित कौटिल्य के विचारों का विवेचन (उल्लेख) कीजिए। (2015)
या
आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारण बताइए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य सम्बन्धी सप्तांग सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। [2010]
या
कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। [2014]
उत्तर
कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों और राजा के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया है। कौटिल्य प्रजा के सुख को सर्वोपरि मानते हैं। यह उनकी विचारधारा का मूल आधार है। उन्होंने लिखा है-
प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हितो हितम्।
नात्मप्रिये हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।
(कौटिल्य अर्थशास्त्र 1:39)
[अर्थात् ‘प्रजा’ के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा का प्रिय और हित ही राजा का प्रिय और हित है।]
इसी आधार पर कौटिल्य राज्य के कार्यक्षेत्र तथा राजा के कर्तव्यों की विशद् विवेचना भी करता है। उनके अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
1. वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना – कौटिल्य के अनुसार राज्य का एक प्रमुख कार्य वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है। प्राचीन भारतीय जीवन के अन्तर्गत चार वर्षों और वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। कौटिल्य का मत है कि “जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रमों के नियमों का पालन करती है और त्रयी (तीन वेद) द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता।”
2. न्याय की व्यवस्था करना – स्वधर्म पालन योजना को कार्यान्वित करने के लिए न्यायव्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। इसके दो क्षेत्र होते हैं-
(i) व्यवहार क्षेत्र तथा (ii) कण्टक शोधन क्षेत्र। पहले का सम्बन्ध नागरिकों के पारस्परिक विवादों से है और दूसरे का राज्य के कर्मचारियों व व्यवसायियों से है। निर्णय के लिए कौटिल्य राज्य को अनेक प्रकार के न्यायालयों की स्थापना का परामर्श देता है।
3. दण्ड की व्यवस्था करना – राज्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य दण्ड की व्यवस्था करना है। दण्ड से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है, उसकी रक्षा होती है, रक्षित वस्तु बढ़ती है और बढ़ी हुई वस्तु का उपभोग होता है। समाज और सामाजिक व्यवहार भी दण्ड पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए दण्ड की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दण्ड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। दण्ड देते समय राज्य को अपराधी की सामर्थ्य, अपराधी का वर्ण, अपराधी के सुधार आदि को ध्यान में रखना चाहिए। यथोचित दण्ड देने वाला राजा पूज्य होता है और केवल यथोचित दण्ड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। यदि दण्ड को उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान निर्बल को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को।
4. राज्य की सुरक्षा करना – राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी रक्षा करे, क्योंकि यदि वह स्वयं अपनी रक्षा न कर सका तो वह नष्ट हो जाएगा। अपनी रक्षा हेतु राज्य को समुचित सेना, सुदृढ़ दुर्गों, पुलों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। षाडगुण्य नीति’ के अन्तर्गत राज्य को वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन के लिए सन्धि, विग्रह (युद्ध), आसन (तटस्थता), यान (शत्रु पर आक्रमण करना), संश्रय (बलवान का आश्रय लेना) तथा दैवीभाव (सन्धि और युद्ध को एक साथ प्रयोग) को आधार बनाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सफल संचालन हेतु राज्य को साम, दाम, दण्ड, भेद साधनों का अनुसरण करना चाहिए।
5. गुप्तचर की व्यवस्था करना – इस कर्त्तव्य के विधिवत् पालन हेतु राज्य के कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के दैनिक व्यवहार पर गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा नजर रखता है। विपत्ति के समय राज्य प्रजा की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जो कि उसका परम कर्तव्य है।
6. लोकहित और सामाजिक कल्याण करना – कौटिल्य राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपता है। इसके अन्तर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों का पालन-पोषण करेगा। असहाय गर्भवतियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का पालन-पोषण करेगा। राज्य के अन्य भी कर्तव्य हैं; जैसे—कृषि के लिए बाँध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना आदि। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर वह खुद किसान को देगा।
राजा के लोकहित और समाज-कल्याण सम्बन्धी इन राज्यों के उल्लेख में कौटिल्य की दूरदर्शिता ही झलकती है। कौटिल्य के अनुसार, खदानें, वस्तुओं के निर्माण, जंगलों में इमली की लकड़ी और हाथियों को प्राप्त करने तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने के प्रबन्ध भी राज्य के ही कार्य हैं।
7. आर्थिक प्रबन्ध करना – कौटिल्य के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और आर्थिक विषयों का प्रबन्ध सुव्यवस्थित रूप में होना चाहिए। राज्य के पास भरा-पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का मत है कि राजा को प्रजा से उपज का छठा भाग लेना चाहिए तथा कोष में बहुमूल्य धातुएँ तथा मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि आवश्यक होने पर राज्य के द्वारा धनवानों पर अधिक कर लगाये जाने चाहिए और इस प्रकार एकत्रित की गयी धनराशि गरीबों में बाँट देनी चाहिए।
8. युद्ध करना – कौटिल्य के अनुसार, युद्ध करना राज्य का प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ का केन्द्र एक ऐसा विजिगीषु (विजय की इच्छा रखने वाला) राजो है जिसका उद्देश्य निरन्तर नये प्रदेश प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदण्ड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती हैं।
कौटिल्य के अनुसार, राजा के द्वारा उपर्युक्त सभी कार्यों को सम्पादन लोकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए।
कौटिल्य राजतन्त्र को शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है। वह राज्य के सात अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। इतना होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। उस पर निम्नलिखित कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता-.
1. अनुबन्धवाद – कौटिल्य के अनुसार, मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की उसके बदले में राजा ने अपनी प्रजा के धन-जन की रक्षा का वचन दिया था। इसीलिए राजा प्रजा के जन-धन को हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकता। कौटिल्य का मत है कि राजा की स्थिति वेतन-भोगी सैनिकों के समान ही होती है, अर्थात् राजा राजकोष से निश्चित वेतन ले सकता है। उसे मनमाने ढंग से राज्य की सम्पत्ति को व्यय करने का अधिकार नहीं था।
2. धर्म और रीति-रिवाज – कौटिल्य के अनुसार, राजा के अधिकार धर्म और रीति-रिवाज सीमित थे और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य था। उसे यह डर रहता था कि राजा द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जनता क्षुब्ध होकर स्वयं ही उसके जीवन का अन्त न कर दे। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक को भये भी राजा को मनमानी करने से रोकता था।
3. मन्त्रिपरिषद् – राजा की शक्ति पर मन्त्रिपरिषद् का भी प्रतिबन्ध होता था। उसके अनुसार राजा और मन्त्रिपरिषद् राज्य रूपी रथ के दो चक्र हैं, इसीलिए मन्त्रिपरिषद् का अधिकार राजा के बराबर ही है। मन्त्रिपरिषद् राजा की शक्ति पर नियन्त्रण रख उसे मनमानी करने से रोकती थी।
4. राजा का व्यक्तित्व और उसकी शिक्षा – राजा का व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गयी शिक्षा भी कौटिल्य के राजा की निरंकुशता पर अत्यन्त प्रभावशाली प्रतिबन्ध है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक गुण आवश्यक बताये हैं और ऐसा सर्वगुणसम्पन्न राजा अपने स्वभाव से निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहे हैं कि वह लोकहित के कार्यों में लगा रहे। श्री कृष्णराव ने ठीक ही कहा है कि “कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है।”
प्रश्न 6.
‘समाजवाद क्या है? यह किन सिद्धान्तों पर आधारित है? किन्हीं तीन सिद्धान्तों को विस्तार से समझाइए। (2007)
या
समाजवाद के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। [2013]
या
समाजवाद के किन्हीं चार सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई और वर्तमान समय में यह विचारधारा बहुत अधिक लोकप्रिय है। समाजवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची ‘Socialism’, *Socius’ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ समाज और जैसा कि शब्द व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाज के महत्त्व पर आधारित है। समाजवाद का आधारभूत उद्देश्य समानता की स्थापना करना है और इस समानता की स्थापना के लिए स्वतन्त्र प्रतियोगिता का अन्त किया जाना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए और उत्पादन व्यवस्था का संचालन किसी एक वर्ग के लाभ को दृष्टि में रखकर नहीं, वरन् सभी वर्गों के सामूहिक हित को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। समाजवाद की परिभाषा करते हुए रॉबर्ट ब्लैकफोर्ड ने कहा है कि समाजवाद के अनुसार भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन सबकी सम्पत्ति रहें और उनका प्रयोग तथा संचालन जनता द्वारा जनता के लिए ही हो।” इसी प्रकार फ्रेड बेमेल ने कहा है। कि “समाजवाद का अर्थ है व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के अधीन रखना।”
समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र – राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में समाजवाद का मत व्यक्तिवाद के नितान्त विपरीत है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किये जाने चाहिए, जो व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हों और क्योंकि व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिए किये जाने वाले कार्यों की कोई सीमा नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं।
साधारणतया यह कहा जा सकता है कि समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य को आन्तरिक एवं बाहरी सुरक्षा-व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का प्रबन्ध एवं अपाहिज और बूढ़े व्यक्तियों की सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।
समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा और पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त विचारधारी और आन्दोलन है। यह समानता को अपना आदर्श मानकर चलता है और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता स्थापित करना चाहता है।
समाजवाद के सिद्धान्त
समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्तों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है-
1. समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बल देता है- समाजवाद का आधारभूत विचार यह है कि व्यक्ति कोई एक अकेला प्राणी नहीं है, वरन् यह समाज के दूसरे व्यक्तियों से उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग परस्पर सम्बन्धित होते हैं।
2. समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करता है- समाजवाद का विचार यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में प्रचलित प्रतियोगिता से धनिक वर्ग को ही लाभ होता, है और श्रमिक वर्ग को हानि। प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक व्यवसायी अपनी वस्तुओं को इतनी सस्ती बेचना चाहता है कि उसकी श्रेष्ठता बिल्कुल नष्ट हो जाती है; अतः समाजवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करना चाहता है।
3. समाजवाद का ध्येय समानता है- समाजवाद वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान असमानता का अत्यन्त विरोधी है और यह नवीन समाज का निर्माण ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहता है कि उसमें वर्तमान समय में विद्यमान गम्भीर असमानता कम-से-कम हो जाए। योग्यता के अन्तर को तो समाजवादी भी स्वीकार करते हैं और वे यह भी मानते हैं कि पूर्ण समानता अनुचित, अनावश्यक और असम्भव है, किन्तु साथ ही उनका लक्ष्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें।
4. समाजवाद का उद्देश्य पूँजीवाद का अन्त है- समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा तथा पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध पर आधारित है। समाजवाद के अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बहुत अधिक अमीर और कुछ लोग बहुत अधिक गरीब हो जाते हैं और इस प्रकार की आर्थिक विषमता से राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। पूँजीवादी व्यवस्था उपभोग और उत्पादन की दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसमें कला तथा प्रतिभा का भी पतन हो जाता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अशान्ति को जन्म देने वाली भी होती है। इस प्रकार समाजवाद के अनुसार वर्तमान समय की पूँजीवादी व्यवस्था दोषपूर्ण, जर्जर, अन्यायी व शोषक है और सम्पूर्ण समाज के हित में इस अर्थव्यवस्था का अन्त कर दिया जाना ही उचित है।
5. समाजवाद एक प्रजातान्त्रिक विचारधारा है- समाजवाद के सम्बन्ध में प्रमुख बात यह है। कि यह एक प्रजातान्त्रिक विचारधारा है। अनेक बार समाजवाद को साम्यवाद का पर्यायवाची मान लिया जाता है, जो नितान्त भ्रमपूर्ण है। पूँजीवाद के विरोध में परस्पर सहमत होते हुए भी समाजवाद और साम्यवाद परस्पर नितान्त विरोधी विचारधाराएँ हैं। इबन्सटीन (Ebenstein) के शब्दों में, “ये (समाजवाद और साम्यवाद) विचार और जीवन के दो नितान्त विरोधी ढंग हैं, उतने ही विरोधी जितने कि उदारवाद और सर्वाधिकारवाद।” इन दोनों विचारधाराओं में प्रमुख भेद साधनों के सम्बन्ध में है। साम्यवाद हिंसक साधनों को अपनाने के पक्ष में है, किन्तु समाजवाद का विचार है कि वांछित परिवर्तन प्रजातन्त्रात्मक और संवैधानिक साधनों से ही लाया जाना चाहिए। समाजवाद प्रजातन्त्रवादी विचार है और साम्यवाद सर्वाधिकारवादी।
6. समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के पक्ष में है- पूँजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी होने के कारण समाजवाद भूमि और उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्त की माँग करता है और उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। समाजवादियों के अनुसार, “वैयक्तिक उद्योग वैयक्तिक लूटमार है और व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामाजिक अथवा सामूहिक सम्पत्ति का रूप देना ही उचित है।
7. समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्राथमिकता देता है- समाजवाद का विचार है कि सम्पूर्ण समाज का सामूहिक हित अकेले व्यक्ति के हित से अधिक मूल्यवान है और आवश्यकता पड़ने पर समष्टि के हित में व्यक्ति के हित का बलिदान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समाजवादियों का विचार है कि सामूहिक हित में व्यक्तिगत हित निहित होता है और सामूहिक हित की साधना से व्यक्तिगत हित की साधना अपने आप ही हो जाती है।
8. समाजवाद राज्य को एक सकारात्मक गुण मानता है- समाजवाद व्यक्तिवाद के इस कथन को अस्वीकार करता है कि राज्य एक आवश्यक दुर्गुण हैं और इसके विपरीत राज्य को एक ऐसी कल्याणकारी संस्था मानता है जिसका जन्म ही नागरिकों के जीवन को सभ्य और सुखी बनाने के लिए होता है। अधिकांश समाजवादी इतिहास से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राज्य संस्था चिरकाल से मानव-जाति की सेवा करती चली आ रही है और यदि इसने कहीं बल का प्रयोग किया भी है तो सामूहिक हित के लिए ही। इस प्रकार साधारणतया समाजवादी राज्य को एक जनहितकारी संस्था मानते हैं।
9. समाजवाद राज्य को अधिकाधिक कार्य सौंपना चाहता है- समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं और व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। समाजवाद के अनुसार, व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी-पूरी भलाई नहीं कर सकता और इस पुलिस राज्य में 99 प्रतिशत जनता पूँजीवादी शोषण से पिसकर अपने प्राण दे देगी। ऐसी स्थिति में गरीबों और मजदूरों के हित में राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित अधिक-से-अधिक कार्य किये जाने चाहिए।
इस प्रकार, समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा वैयक्तिक हित के स्थान पर सामूहिक हित और प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करके, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियन्त्रण के आधार पर आर्थिक समानता स्थापित कराने का प्रयत्न किया जाता है।
प्रश्न 7.
लोकतान्त्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
या
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लोकतान्त्रिक समाजवाद पर एक लेख लिखिए।
उत्तर
‘लोकतन्त्रवाद’ और ‘समाजवाद’ के संयोग से जिस उदार समाजवाद की रचना हुई उसे ही लोकतान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) कहा जाता है। आज के युग में जबकि पश्चिमी पूँजीवादी लोकतन्त्र चीनी उग्र साम्यवाद से लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है, लोकतान्त्रिक समाजवाद दक्षिण और वाम दोनों ही विचारों को सामंजस्य करते हुए एक मध्यममार्गी समाजवाद का रूप ले रहा है। फ्रांस, इंग्लैण्ड, इटली और अब भारत में भी इसी प्रकार के समाजवाद का रूप विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपना रास्ता तय किया। कांग्रेस द्वारा समाजवादी व्यवस्था को अपना लक्ष्य घोषित कराने में नेहरू जी की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है।
पण्डित नेहरू का लोकतान्त्रिक समाजवाद
1. लोकतन्त्र के समर्थक – यद्यपि भारत में समाजवाद का प्रचार करने में कांग्रेसी समाजवादियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, किन्तु वह नेहरू जी की भूमिका के सामने फीकी पड़ जाती है। जब वे इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब वे वहाँ की लोकतन्त्र व्यवस्था से काफी प्रभावित हुए। उन्हें लोकतन्त्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ने काफी प्रभावित किया। वे रूस भी गये तथा वहाँ की समाजवादी व्यवस्था से भी वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। वहाँ की वर्ग-विहीन समाज व्यवस्था से वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। परन्तु उसके साधनों में उन्हें हिंसा-ही-हिंसा दिखायी दी। अतः उन्होंने माक्र्सवाद या साम्यवाद को ज्यों-का-त्यों स्वीकार न करके वर्ग-सहयोग एवं सामंजस्य पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने समाजवाद और लोकतन्त्र का मध्य मार्ग अपनाकर उसे ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद का नाम दिया।
2. लोकतन्त्र समाजवाद को लाने का साधन – नेहरू जी ने लोकतन्त्र व समाजवाद को एक- दूसरे को पूरक माना है। वे लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक होने के साथ-साथ समाजवाद के भी बड़े प्रशंसक थे। उनका कहना था कि भारत में जब तक समानता नहीं आयेगी, तब तक लोकतन्त्र की स्थापना सम्भव नहीं है। लोकतन्त्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक समानता आवश्यक है। एक ओर उच्च वर्ग तथा दूसरी ओर दलित वर्ग जब तक समान स्तर पर नहीं लाये जायेंगे तब तक लोकतन्त्र कदापि सम्भव नहीं है। वे समाजवाद को लाने के लिए लोकतन्त्र को प्रमुख साधन मानते थे।
3. संघर्ष एवं हिंसा का विरोध – यद्यपि नेहरू जी मार्क्स के सिद्धान्तों की बड़ी प्रशंसा करते थे, किन्तु वे अहिंसा द्वारा समाजवाद को भारत में लाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतन्त्र के अभाव में राजनीतिक लोकतन्त्र का कोई मूल्य नहीं होता, परन्तु इसके लिए वे संघर्ष एवं हिंसा को साधन नहीं बनाना चाहते थे। वे हिंसात्मक रवैये को एकदम ‘अवैज्ञानिक’, ‘तर्कहीन’ तथा ‘असभ्य’ समझते थे। उनकी धारणा यह थी कि समाज की प्रमुख समस्याओं का कोई भी समाधान हिंसा के द्वारा नहीं किया जा सकती। इसका स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि उन पर गाँधी जी का प्रभाव विशेष रूप से अधिक था। वे गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित शान्तिपूर्ण उपायों में विश्वास रखते थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करके तथा समाज में विद्यमान असमानताओं को कम करके सब लोगों को प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान करने वाले समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति शान्तिपूर्ण संवैधानिक साधनों से ही होनी चाहिए।
4. लोकतन्त्र की प्रथम शर्त दरिद्रता, असमानता एवं अशिक्षा को समाप्त करना – नेहरू जी लोकतन्त्र के आर्थिक पक्ष के महत्त्व को स्वीकार करते थे। उनका विचार था कि स्वराज्य को यथार्थ रूप देने के लिए राष्ट्र के धन का समुचित एवं न्यायपूर्ण वितरण किया जाए तथा समाज में विद्यमान वर्ग विभेद को समाप्त किया जाए। शिक्षा के माध्यम से शिक्षित एवं अशिक्षित जनता के अन्तर को दूर किया जाए। दरिद्रता, असमानता एवं अशिक्षा को समाप्त करना वे लोकतन्त्र के लिए प्रथम शर्त मानते थे।
भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद
यदि आज भारत की जनता ने लोकतान्त्रिक समाजवाद’ को अपना मान लिया है तथा ‘समाजवाद’ शब्द सम्माननीय एवं सुन्दर हो गया है और यदि इसका अर्थ ‘उग्र वर्ग-संघर्ष’ तथा ‘सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के स्थान पर ‘विकास’, ‘कल्याण तथा सामाजिक जीवन में ईमानदारी’, ‘पवित्रता’ एवं ‘अनुशासन’ लगाया जाने लगा है तो इसका श्रेय साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल अथवा समाजवादी दल को ही नहीं बल्कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू को है। उन्होंने ही अपने प्रयासों द्वारा लोकतन्त्र एवं समाजवाद का समन्वय करके इस नवीन विचारधारा को जन्म दिया। यद्यपि वे मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के पक्षपाती थे, किन्तु वे मार्क्सवादी या साम्यवादी नहीं थे। उन्होंने मार्क्सवाद के समाजवादी पक्ष को कुछ संशोधन कर स्वीकार किया है। उनके इन्हीं विचारों को भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा नीति-निदेशक सिद्धान्तों में स्थान दिया गया है। शासन के द्वारा अपनायी गई पंचवर्षीय योजनाओं में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद के लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया गया। नेहरू जी का विचार था कि “नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा ही हम समाजवाद को प्राप्त कर सकते हैं; अतः हमारे देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन (Economic Planning) की नीति को अपनाया गया है। वास्तव में नेहरू जी का चिन्तनपूर्ण रूप से व्यावहारिक कहा जा सकता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)
प्रश्न 1.
समाजवादी राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [2007]
या
समाजवादी राज्य के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [2010]
उत्तर
समाजवाद की आलोचना
आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था के अन्त के लिए समाजवाद एक सुन्दर मार्ग प्रस्तुत करता है। समाजवाद ने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामाजिक हित को उच्चतर स्थान प्रदान कर प्रशंसनीय कार्य किया है, किन्तु इन गुणों के होते हुए भी समाजवादी व्यवस्था दोषमुक्त नहीं है। इस व्यवस्था की प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है-
1. उत्पादन क्षमता में कमी – यह मानव स्वभाव है कि व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा पर ही वह ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन कार्य राज्य के हाथ में आ जाने और सभी व्यक्तियों को पारिश्रमिक निश्चित होने के कारण कार्य करने के लिए प्रेरणा का अन्त हो जाता है और व्यक्ति आलसी बन जाता है। इसी कारण आर्थिक प्रगति रुक जाती है।
2. नौकरशाही का विकास समाजवादी – व्यवस्था में सभी उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण होगा और उनका प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के हाथ में शक्ति आ जाने का स्वाभाविक परिणाम नौकरशाही का विकास होगा। काम की गति शिथिल हो जाएगी, सरल-से-सरल काम देर से होंगे और घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
3. समानता की धारणा प्राकृतिक विधान के विरुद्ध – समाजवाद समानता, सबसे प्रमुख रूप में आर्थिक समानता पर बल देता है और आलोचकों के अनुसार समानता का यह विचार प्राकृतिक विधान और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। प्रकृति के द्वारा व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियाँ समान रूप में नहीं वरन् असमान रूप में प्रदान की गयी हैं और इसी कारण समानता स्थापित करने के किसी भी प्रयत्न में सफलता प्राप्त होमा बहुत अधिक सन्देहपूर्ण है।
4. राज्य की कार्यकुशलता में कमी – समाजवादी व्यवस्था में राज्य के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो जाने के कारण राज्य की कार्यकुशलता में भी कमी हो जाएगी। समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी, उत्पादन, वितरण तथा श्रमिक विधान सम्बन्धी सभी कार्य राज्य द्वारा होंगे। आलोचकों का कथन है कि राज्य के हाथ में इतने अधिक कार्यों के आ जाने से एक भी कार्य ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं हो सकेगा।
5. मनुष्य का नैतिक पतन – सभी कार्यों को करने की शक्ति राज्य के हाथ में आ जाने से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, साहस और आरम्भक के नैतिक गुणों का व्यक्तियों में अन्त हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में उसे अपने विकास की नवीन दिशाएँ और देशाएँ न प्राप्त होने के कारण वह हतप्रभ हो जाएगा और उसका नैतिक पतन हो जाएगा।
6. समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होगी – आलोचके यह भी कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से बहुत अधिक खर्चीली होगी। जब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो एक छोटे-से काम के लिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं और फिर भी यह कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाता।
7. व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्त का भय – समाजवाद के अन्तर्गत जब सरकार के द्वारा बहुत अधिक कार्य किये जाते हैं तो इस बात का भय रहता है कि व्यक्तियों के जीवन में सरकार के इस अत्यधिक हस्तक्षेप से उनकी स्वतन्त्रता का अन्त हो जाएगा।
प्रश्न 2.
व्यक्तिवाद और समाजवाद का अन्तर समझाइए। उद्योगों के निजीकरण की प्रवृत्ति इन दोनों में से किसकी अवधारणा के प्रतिकूल है? कारण का भी उल्लेख कीजिए। [2007]
उत्तर
व्यक्तिवाद और समाजवाद का अन्तर
1. विचारधारा – व्यक्तिवादी सिद्धान्त के समर्थक व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। उनके अनुसार, राज्य के कार्य तथा कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करते हैं; अत: राज्य के कार्यों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। वे राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। । दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किये जाने चाहिए जो व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हों। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के कार्यों की कोई सीमा नहीं है तथा सामाजिक जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं।
2. कार्यक्षेत्र- व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक-से-अधिक सीमित कर दिया जाए। स्पेन्सर के मतानुसार, “व्यक्ति का स्थान समाज तथा राज्य के ऊपर होना चाहिए।
और राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जिन्हें व्यक्ति नहीं कर सकता।” उनके अनुसार राज्य के केवल तीन निम्नलिखित कार्य होने चाहिए-
- आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था करना,
- देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना तथा
- न्याय और दण्ड की व्यवस्था करना।
दूसरी ओर समाजवादी समानता को अपना आदर्श मानकर चलते हैं और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अधिकाधिक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष बल देते हैं–
- समाज की आंगिक एकता,
- समाज में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग,
- पूँजीवाद का अन्त तथा
- उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व।
उद्योगों के प्रति दृष्टिकोण
व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के कार्यों को न्यूनतम कर देना चाहती है तथा उद्योगों को व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से खुला रखना चाहती है। वह उद्योगों की स्थापना, संचालन तथा विकासे में राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहती। वह खुली प्रतियोगिता में विश्वास रखती है तथा एक प्रकार से पूँजीवाद की समर्थक है।
दूसरी ओर समाजवादी विचारधारा पूँजीवाद की घोर विरोधी होने के कारण भूमि और उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्त की माँग करती है। यह विचारधारा उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहती है। समाजवादी विचारधारा के अनुसार वैयक्तिक उद्योग वैयक्तिक लूटमार है और व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामाजिक अथवा सामूहिक सम्पत्ति का रूप देना ही उचित है।
अतः निष्कर्षतया कहा जा सकता है कि उद्योगों के निजीकरण की प्रवृत्ति समाजवादी विचारधारा के प्रतिकूल है।
प्रश्न 3.
राज्य से सम्बन्धित मनु व कौटिल्य के सप्तांग सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
या
आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धान्त के अनुसार राज्य के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखिए। [2012, 13]
उत्तर
भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के अन्तर्गत मनु और कौटिल्य दो जाज्वल्यमान क्षेत्र हैं तथा इन दोनों की विचारधारा एक-दूसरे के बहुत अधिक समान है। मनुस्मृति (जिसे कि हिन्दू विधि की सम्पूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है।) के अन्तर्गत राज्य के सावयव स्वरूप (Organic form) की चर्चा की गई है; अर्थात् इसके राज्य की कल्पना जीवित जाग्रत शरीर के रूप में की गई है तथा राज्य को सप्तांगी माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार, राज्य के सात । अंग इस प्रकार हैं—(1) स्वामी (राजा), (2) मन्त्री, (3) पुर, (4) राष्ट्र, (5) कोष, (6) दण्ड तथा (7) मित्र। मनुस्मृति में चारों दिशाओं में व्याप्त एक विशाल राज्य का चित्र खींचा गया है जिसके आधार पर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है, अथवा यह सम्भावना की जा सकती है। कि इस ग्रन्थ की रचना के समय एक सुविशाल प्रदेश को राजनीतिक एकता प्राप्त हो चुकी थी। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने ग्रन्थ ‘अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धान्त का वर्णन किया है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार भी राज्य का निर्माण सप्त अंगों अथवा तत्त्वों से मिलकर हुआ है।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य की संरचना, प्रकार्यों एवं प्रकृति का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उद्देश्य से मनु एवं कौटिल्य दोनों ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है; अर्थात् उसे एक जीवित शरीर के रूप में निरूपित किया है तथा उसके सात अंग बताये हैं। राज्य के इन सात अंगों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-
1. स्वामी – मनु और कौटिल्य दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य के समस्त अंगों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंग स्वामी अथवा राजा है, परन्तु उसे निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं, अपितु धर्म के अधीन माना गया है।
2. मन्त्री अथवा आमात्य – राजा की सहायता एवं उसे परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
3. पुर अथवा दुर्ग – यह कहा गया है कि सैन्य शक्ति का प्रयोग पुर अथवा दुर्ग से ही भली भॉति सम्भव है। यह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक है। जिसका दुर्ग सुदृढ़ होता है उस राज्य को परास्त करना सरल नहीं है।
4. जनपद – जनपद में जनता तथा भूमि के भागों को सम्मिलित किया गया है।
5. कोष – राज्य की शक्ति एवं उसकी सुदृढ़ता के लिए एक धन-धान्य से पूर्ण राजकोष होना चाहिए तथा उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह आपातकाल में राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
6. दण्ड अथवा सेना – राज्य की सुरक्षा के लिए दण्ड अथवा सेना का विशिष्ट महत्त्व होता है। सुरक्षा एवं आक्रामक-नीति दोनों को अपनाने के लिए एक प्रशिक्षित, अनुशासित, राष्ट्रभक्त तथा निष्ठावान सेना होनी चाहिए।
7. मित्रराष्ट्र की शक्ति के लिए उसके मित्र – राष्ट्रों की संख्या अधिकाधिक होनी चाहिए। | इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु तथा कौटिल्य की विचारधारा एक-दूसरे के बहुत-कुछ समान है तथा दोनों ने सप्तांग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

प्रश्न 4.
समाजवाद के विरोध में तर्क दीजिए।
उत्तर
समाजवाद के विरोध में तर्क निम्नवत् हैं-
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अन्त – राज्य के कार्य-क्षेत्र का विस्तार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्त का परिचायक है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएँ राज्य द्वारा नियन्त्रित होती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वतन्त्र होने के स्थान पर राज्य का गुलाम बन जाता है। हेयक ने उचित ही कहा है, “पूर्ण नियोजन का आशय पूर्ण गुलामी है।”
- पूर्ण समानता असम्भव – समाजवाद समानता पर आधारित विचारधारा है। प्रकृति ने समस्त व्यक्तियों को समान उत्पन्न नहीं किया। जन्म से कुछ व्यक्ति बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख, कुछ स्वस्थ तो कुछ अस्वस्थ, कुछ परिश्रमी तो कुछ आलसी होते हैं। इन सभी को समान समझना प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना करना है। पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती।
- कार्य करने की प्रेरणा का अन्त – व्यक्तियों को श्रम करने की प्रेरणा इस भावना से मिलती है कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति का संचय कर सकेंगे। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राजकीय नियन्त्रण का परिणाम यह होता है कि व्यक्तियों में कार्य करने की प्रेरणा का अन्त हो जाता है।
- नौकरशाही का महत्त्व – समाजवाद में राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी होने के कारण नौकरशाही का महत्त्व बढ़ता है तथा समस्त फैसले शासकीय कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं। वह जन इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की इतनी चिन्ता नहीं करते जितनी अपने स्वार्थों की। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।
- समाजवाद से हिंसा को बढावा – समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रान्तिकारी तथा हिंसात्मक मॉग को अपनाता है। वह शान्तिपूर्ण तरीकों में आस्था नहीं रखता। समाजवाद के द्वारा वर्ग-संघर्ष पर बल देने के परिणामस्वरूप समाज में विभाजन एवं वैमनस्यता की भावना फैलती है।
- उत्पादन का श्रेय श्रमिकों को देना त्रुटिपूर्ण – उत्पादन का श्रेय केवल श्रमिकों को देना न्यायसंगत नहीं है। उत्पादन में श्रम के अलावा पूँजी तथा संसाधन इत्यादि भी आवश्यक होते हैं तथा स्थूल रूप में इन सभी को पूँजी ही कहा जा सकता है।
- समाजवाद लोकतन्त्र विरोधी – समाजवाद की प्रवृत्ति जहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाती है, वहीं लोकतन्त्र का आधार ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता है। लोकतन्त्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यन्त उत्तम स्थान प्राप्त है, जबकि समाजवाद में वह राज्यरूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पुर्जा बन जाता है।
- उग्र राष्ट्रीयता का विकास – समाजवाद किसी राष्ट्रीय सीमा पर विश्वास नहीं करता। वह विश्व के सर्वहारा वर्ग को एक झण्डे के नीचे इकट्ठा करना चाहता है तथा राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठाकर श्रमिकों को राज्य से लड़ाना चाहता है। मार्क्स के अनुसार, “राज्य ने सदैव ही पूँजीपतियों, सामन्तों तथा शोषक वर्ग का साथ दिया है। आज राष्ट्रवाद प्रधान और समाजवाद गौण है।’
प्रश्न 5.
क्या भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। इसके पक्ष में किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख कीजिए। [2012]
उत्तर
कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जनता का कल्याण किया जाता है, किसी वर्ग विशेष का नहीं। पं० नेहरू के अनुसार, “सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अन्तर को समाप्त करना तथा जीवन-स्तर को उठाना लोक-कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्त्व हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विकास की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया है। इसके पक्ष में दो तर्क इस प्रकार हैं-
- भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए नीति-निदेशक तत्त्वों को सम्मिलित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रम प्रदान करने का निश्चय किया गया है।
- लोक-कल्याणकारी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप देने की दृष्टि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके अनुसार भारतीय समाज और भारतीय नागरिकों के चतुर्मुखी विकास की दिशा में अनेक उपयोगी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)
प्रश्न 1.
समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र बताइए।
या
समाजवादी राज्य के कार्यों का परीक्षण कीजिए। [2010]
उत्तर
राज्य के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने की दृष्टि से समाजवादी सिद्धान्त व्यक्तिवादी सिद्धान्त के ठीक विपरीत है। व्यक्तिवाद जहाँ राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र पर बल देता है वहीं समाजवाद राज्य के उन समस्त कार्यों को सम्पादित करने को कहता है, जिनसे समाज की उन्नति सम्भव है। इसके अतिरिक्त समाजवाद की मान्यता है कि राज्य को उत्पत्ति एवं वितरण के साधनों पर नियन्त्रण रखकर स्वयं ही सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि समाजवाद के अनुसार प्रायः सामाजिक जीवन के समस्त कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस सम्बन्ध में गार्नर का यह कथन उचित ही है, “राज्य मानव विकास की सर्वोच्च संस्था है। उसका कार्यक्षेत्र व्यापक है। वह व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं नैतिक सभी क्षेत्रों के हितों की अभिवृद्धि करती है।”
प्रश्न 2.
“लोक-कल्याणकारी राज्य न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।
उत्तर
प्रत्येक व्यक्ति को इतना पारिश्रमिक तो अवश्य ही मिलना चाहिए कि वह न्यूनतम जीवन-स्तर के अनुसार अपने जीवन-यापन हेतु आवश्यक सामग्री तथा सुविधाएँ प्राप्त कर सके। इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्री क्राउथर ने लिखा है कि “नागरिकों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु पर्याप्त भोजन-व्यवस्था होनी चाहिए। निवास, वस्त्र इत्यादि के न्यूनतम जीवन-स्तर की ओर से उन्हें चिन्तारहित होना चाहिए। शिक्षा की उन्हें पूर्ण तथा समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। उन्हें जीवन का आनन्द भोगने हेतु अवकाश एवं साधन मिलने चाहिए। बेरोजगारी तथा वृद्धावस्था के दु:ख से उनकी रक्षा करनी चाहिए।’
प्रश्न 3.
कौटिल्य के अनुसार राज्य को कौन-से लोकहितकारी कार्य करने चाहिए?
उत्तर
कौटिल्य ने राज्य को लोकहित तथा सामाजिक कल्याण के कार्य सौंपे हैं। लोक-कल्याण सम्बन्धी जिन कार्यों को राजा सम्पन्न करता है उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं|
- जीविकोपार्जन के साधनों का नियमन।
- चिकित्सालयों का निर्माण।
- वृद्ध, असहाय, अनाथ, विधवा, दुःखियों तथा रोगियों की सहायता।
- कृषि, पशुपालन, उद्योग, वाणिज्य इत्यादि का विकास।
- बाँधों का निर्माण, जलमार्ग, जलाशय, स्थलमार्ग एवं बाजार बनाना।
- दुर्भिक्ष के समय जनसाधारण की सहायता।
- पण्डितों का आदर एवं सम्मान।
- ज्ञान के अनुसन्धान कार्य में लगे आश्रमवासियों एवं विद्यार्थियों की रक्षा।
- आवश्यक होने पर धनवानों से अधिक कर वसूलकर गरीबों में वितरित करना।
- जंगलों की रक्षा करना।
- मानव के चारों उद्देश्यों अर्थात् धर्म, काम, मोक्ष एवं अर्थ की सिद्धि में सहायता करना।
प्रश्न 4.
आधुनिक राज्य के चार प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। [2013, 14]
उत्तर
आधुनिक राज्य के चार प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
- शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना,
- देश की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा,
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना,
- न्याय एवं दण्ड की व्यवस्था।
प्रश्न 5.
व्यक्तिवादी विचारधारा के अन्तर्गत गिलक्रिस्ट ने राज्य का कार्यक्षेत्र किस प्रकार निर्धारित किया है?
उत्तर
व्यक्तिवादी विचारधारा के अन्तर्गत गिलक्रिस्ट ने राज्य का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया है
- देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना,
- राज्य एवं राज्य के नागरिकों की बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा,
- नागरिकों की मानहानि से रक्षा,
- नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति इत्यादि की सुरक्षा तथा
- अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दण्डित करना।
प्रश्न 6.
व्यक्तिवाद की चार विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की चार प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है।
- व्यक्तिवाद राज्य को साधन मानता है।
- यह व्यक्ति को साध्य अथवा लक्ष्य मानता है तथा व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है।
- व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अत्यधिक बल देता है।
प्रश्न 7.
आर्थर स्लेशिंगर तथा गार्नर ने कल्याणकारी राज्य की क्या परिभाषा दी है?
उत्तर
आर्थर स्लेशिंगर के शब्दों में, “कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शासन अपने समस्त नागरिकों हेतु रोजगार, आय, चिकित्सा, शिक्षा, सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं आवास के कुछ स्तर स्थापित करने हेतु तैयार रहता है।”
गार्नर के मतानुसार, “कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा जीवन में भौतिक तथा नैतिक स्तर को विस्तृत करना है।”
प्रश्न 8.
लोक-कल्याणकारी राज्य अपने कार्यक्षेत्र में कैसे वृद्धि कर लेता है?
उत्तर
लोक-कल्याणकारी राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है। वस्तुतः यह सिद्धान्त व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस आदर्श पर आधारित है कि राज्य को वह समस्त कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट अथवा कम नहीं होती। इसी आधार पर एम०जी० हॉब्सन ने लिखा है कि राज्य ने एक डॉक्टर, एक नर्स, स्कूल मास्टर, व्यापारी, उत्पादक, बीमा एजेण्ट, मकान बनाने वाले मिस्त्री, नगर योजना तैयार करने वाले, रेलवे नियन्त्रक इत्यादि सैकड़ों अन्य लोगों के कार्यों के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है।”
प्रश्न 9.
समाजवाद के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। [2013]
उत्तर
समाजवाद की विचारधारा की उत्पत्ति व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई और वर्तमान समय में यह विचारधारा बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसके दो गुण निम्नवत् हैं-
1. समाजवाद भ्रातृत्व तथा समाज-सेवा भाव को बढ़ाता है- समाजवादी राज्य समानता पर आधारित होगा। यह राज्य सामूहिक हानि-लाभ के विचार को ध्यान में रखते हुए भ्रातृत्व की ओर अग्रसर होगा। व्यक्तियों पर समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और इस बात की आशा की जा सकती है कि समाजवादी व्यवस्था में उनकी प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थों की तुष्टि के स्थान पर सामूहिक हितों की साधना ही हो जाएगी।
2. समाजवाद एक न्यायपूर्ण तथा जनतान्त्रिक विचारधारा है- राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद जनतन्त्र के प्रति विश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि राजतन्त्रीय या कुलीनतन्त्रीय व्यवस्था में अनिवार्य रूप से विद्यमान भेद समाजवाद को मान्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त समाजवाद उत्पादन पर ‘सामूहिक स्वामित्व’ और उसकी सामूहिक व्यवस्था का समर्थक है, जो पूर्णतया प्रजातान्त्रिक तथा न्यायोचित विचार है। वास्तव में प्रजातन्त्र और समाजवाद परस्पर पूरक हैं जिनमें से एक राजनीतिक समानता का प्रतिपादन करता है तो दूसरा आर्थिक समानता का। लैडलर के शब्दों में, “प्रजातान्त्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है।”
प्रश्न 10.
धर्म-निरपेक्ष राज्य के दो लक्षण बताइए। [2012]
उत्तर
- धर्म-निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न धर्म-विरोधी, अपितु वह धार्मिक संकीर्णताओं एवं वृत्तियों से बिल्कुल दूर धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ होता है।
- धर्म-निरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष को प्रधानता प्रदान नहीं करता। धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर वह न तो किसी की सहायता करता है और न ही किसी नागरिक को सरकारी पद से वंचित करता है।
प्रश्न 11.
समाजवाद तथा लोक-कल्याणकारी राज्यों में दो अन्तर लिखिए। [2007, 10]
उत्तर
समाजवाद एवं लोक-कल्याणकारी राज्यों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो अन्तर हैं-
1. लोक-कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी एवं अधिकतम आर्थिक समानता से है।
समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है यद्यपि समानता का यह विचार प्राकृतिक विधान और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। समाजवाद का आर्थिक समानता का विचार पूँजीवाद के अन्त में निहित है।
2. समाजवाद राज्य को अधिकाधिक कार्य सौंपना चाहता है। समाजवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। इसके विपरीत कल्याणकारी राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य सौंपना चाहते हैं जिनके करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होती। लोक-कल्याणकारी राज्य नागरिक स्वतन्त्रताओं के हिमायती हैं।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
राज्य के कार्यो सम्बन्धी किन्हीं दो सिद्धान्तों के नाम बताइए। (2010)
उत्तर
- समाजवाद तथा
- व्यक्तिवाद।
प्रश्न 2.
राज्य के कार्यों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है ? [2008]
उत्तर
- आवश्यक या अनिवार्य कार्य,
- ऐच्छिक कार्य।
प्रश्न 3.
राज्य के दो अनिवार्य कार्य लिखिए। [2008, 11, 186]
उत्तर
- आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखना तथा
- देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना।
प्रश्न 4.
राज्य के दो ऐच्छिक कार्य बताइए। [2016]
उत्तर
- शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा
- उद्योग-धन्धों और व्यापार का विकास करना।
प्रश्न 5.
“राज्य एक आवश्यक बुराई है।” राज्य के बारे में यह विचारधारा किस सिद्धान्त से सम्बन्धित है? [2010]
उत्तर
व्यक्तिवाद से।
प्रश्न 6.
व्यक्तिवाद के किन्हीं दो समर्थकों के नाम लिखिए।
उत्तर
- जे०एस० मिल तथा
- हरबर्ट स्पेन्सर।
प्रश्न 7.
व्यक्तिवाद के दो गुण लिखिए।
उत्तर
- व्यक्ति को प्रमुखता तथा
- राज्य के कार्यों पर नियन्त्रण।
प्रश्न 8.
राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धान्त के विरुद्ध दो तर्क दीजिए।
उत्तर
- राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है तथा
- राज्य एक आवश्यक बुराई न होकर सकारात्मक अच्छाई है।
प्रश्न 9.
राज्य की सम्प्रभुता को अस्वीकार करने वाले सिद्धान्त का नाम लिखिए।
उत्तर-
राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धान्त।
प्रश्न 10.
आदर्शवाद के सिद्धान्त की दो मुख्य बातें बताइए। [2007]
उत्तर
- राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है तथा
- राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा
प्रश्न 11.
समाजवाद के दो समर्थकों के नाम लिखिए।
उत्तर
- कार्ल माक्र्स तथा
- जयप्रकाश नारायण।
प्रश्न 12.
समाजवाद के दो लक्षण बताइए। [2012]
उत्तर
- व्यक्तिवाद का विरोध
- समानता का समर्थन।
प्रश्न 13.
समाजवाद के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2014, 16]
उत्तर
- यह न्याय पर आधारित है तथा
- यह अधिक लोकतन्त्रात्मक है।
प्रश्न 14.
समाजवाद के दो दोष लिखिए।
उत्तर
- सरकार की शक्ति में अधिक वृद्धि तथा
- धर्म का विरोध।
प्रश्न 15.
समाजवाद की कोई दो मान्यताएँ बताइए।
उत्तर
- व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्राथमिकता तथा
- उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व।
प्रश्न 16.
लोक-कल्याणकारी राज्य की कोई एक परिभाषा लिखिए।
या
लोक-कल्याणकारी राज्य क्या है? [2014]
उत्तर
“लोक-कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत मात्रा में नागरिक सेवाएँ प्रदान करता है।’
प्रश्न 17.
लोक-कल्याणकारी राज्य के दो कार्य लिखिए। [2010, 14]
उत्तर
- लोक-कल्याणकारी राज्य नागरिकों के न्यूनतम सामाजिक जीवन-स्तर को बनाये रखने का प्रयास करता है तथा
- लोक-कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराकर धनी और निर्धन के मध्य अन्तर को कम करता है।
प्रश्न 18.
कल्याणकारी राज्य के दो उद्देश्य लिखिए।
उत्तर
- आर्थिक सुरक्षा तथा
- न्याय की व्यवस्था।
प्रश्न 19.
लोक-कल्याणकारी राज्य के दो लक्षण (विशेषताएँ) बताइए। [2014]
उत्तर
- यह व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है तथा
- यह समाज की सर्वव्यापी उन्नति का प्रयास करता है।
प्रश्न 20.
कल्याणकारी राज्य के दो दोष लिखिए।
उत्तर
- यह सामाजिक सुरक्षा देकर कार्य कर सकने योग्य वृद्धों को निष्क्रिय बना देती है। तथा
- इससे सरकार की शक्ति में अधिक वृद्धि हो जाती है।
प्रश्न 21
कल्याणकारी राज्य के दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर
- भारत तथा
- ग्रेट ब्रिटेन।
प्रश्न 22.
मनु के अनुसार राज्य के दो कार्य बताइए।
उत्तर
- बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा तथा
- असहायों की सहायता करना।
प्रश्न 23.
कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य बढ़ते हैं या घटते हैं?
उत्तर
कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है।
प्रश्न 24.
सामान्य इच्छा (General will) के सिद्धान्त के प्रतिपादक का नाम बताइए।
उत्तर
रूसो।
प्रश्न 25.
मनु द्वारा बताये गये करों के प्रकार बताइए।
उत्तर
- बलि (विभिन्न प्रकार के कर),
- शुल्क (चुंगी),
- दण्ड (जुर्माना) तथा
- भाग (लगान)।
प्रश्न 26.
क्यों मनु की जनता राजा का विरोध कर सकती है?
उत्तर
मनु की जनता राजा का विरोध कर सकती है, उसे गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है।
प्रश्न 27.
कौटिल्य द्वारा बताये गये राज्य के दो प्रमुख कार्य लिखिए।
उत्तर
- वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना तथा
- दण्ड की व्यवस्था करना।
प्रश्न 28.
कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या लिखिए। [2010]
उत्तर
कौटिल्य ने राज्य के सात अंग बताए हैं।
प्रश्न 29.
मनु द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम लिखिए। [2012]
उत्तर
मनु द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम है- मनुस्मृति।
प्रश्न 30.
कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम बताइए। [2010]
उत्तर
कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम है-अर्थशास्त्र
प्रश्न 31.
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है ? (2007)
उत्तर
कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है।
प्रश्न 32.
‘व्यक्तिवाद’ की कोई एक परिभाषा लिखिए।
उत्तर
हम्बोल्ट ने व्यक्तिवाद की यह परिभाषा दी है, “व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों का समर्थक है। यह मनुष्य की क्षमताओं के पूर्ण विकास एवं उसके सभी अधिकारों का एक व्यक्ति होने के नाते उपयोग करने का समर्थन करता है।
प्रश्न 33.
व्यक्तिवाद सिद्धान्त के समर्थक किस बात पर सर्वाधिक बल देते हैं ?
उत्तर
व्यक्तिवाद सिद्धान्त के समर्थक व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं।
प्रश्न 34.
आदर्शवादी विचारधारा की दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर
- राज्य साध्य है, साधन नहीं तथा
- राज्य सर्वशक्तिमान तथा अनिवार्य है।
प्रश्न 35.
आदर्शवाद वे व्यक्तिवाद में मुख्य अन्तर क्या है?
उत्तर
आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य है, जबकि व्यक्तिवाद इसे साधन मानता है।
प्रश्न 36.
राज्य के समाजवादी सिद्धान्त के पक्ष में दो तर्क दीजिए। [2016]
उत्तर
- समाजवाद श्रमिकों एवं गरीबों के शोषण का विरोध करता है तथा
- समाजवाद श्रम तथा समाज सेवा पर अत्यधिक जोर देता है।
प्रश्न 37.
व्यक्तिवादियों के अनुसार, राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कौन-सा है?
उत्तर
व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य समाज में व्याप्त बुराइयों वे कुरीतियों को दूर रखना है।
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
1. “वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है।” यह कथन किसका है? [2014]
(क) हरबर्ट स्पेन्सर का
(ख) रिकार्डों का
(ग) फ्रीमैन का
(घ) माल्थस का
2. निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? [2012, 14]
(क) लॉक
(ख) हीगल
(ग) मिल
(घ) बेन्थम
3. मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं ? [2012]
(क) 4
(ख) 7
(ग) 8
(घ) 9
4. निम्नांकित में से कौन व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक है?
(क) मैकाइवर
(ख) जे०एस० मिल।
(ग) बेन्थम
(घ) प्रो० विलोबी
5. निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है?
(क) सुकरात
(ख) हरबर्ट स्पेन्सर
(ग) टी०एच० ग्रीन
(घ) महात्मा गाँधी।
6. “प्रजा के सुख में ही राज्य का सुख है, प्रजाहित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग कोई सुख नहीं।” यह कथन किसका है?
(क) मनु का
(ख) कौटिल्य का
(ग) सुकरात का
(घ) अरस्तू का
7. वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक (जनक) कौन था?
(क) माओत्से तुंग
(ख) कार्ल माक्र्स
(ग) लेनिन
(घ) स्टालिन
8. “राज्य एक अनावश्यक बुराई है।” यह कथन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? [2007, 13]
(क) व्यक्तिवाद
(ख) अराजकतावाद
(ग) समाजवाद
(घ) आदर्शवाद
9. “वह सरकार सबसे अच्छी है, जो सबसे कम शासन करती है।” यह कौन-सी अवधारणा [2007, 10, 12, 15]
(क) आदर्शवादी
(ख) समाजवादी
(ग) व्यक्तिवादी
(घ) गाँधीवादी
10. राज्य एक आवश्यक बुराई है।’ यह किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है- [2010, 12, 13]
(क) समाजवाद
(ख) अराजकतावाद
(ग) व्यक्तिवाद
(घ) आदर्शवाद
11. ‘अर्थशास्त्र’ का लेखक कौन है ? [2009, 14]
(क) मनु
(ख) शुक्राचार्य
(ग) कौटिल्य
(घ) भीष्म
12. निम्नलिखित में से कौन समाजवादी चिन्तक नहीं है?
(क) जयप्रकाश नारायण
(ख) आचार्य नरेन्द्र देव
(ग) राममनोहर लोहिया
(घ) डॉ० बी०आर० अम्बेडकर
13. कौटिल्य के अनुसार, राज्य के कितने अंग होते हैं ? [2007, 08, 10, 12, 14]
(क) चार
(ख) पाँच
(ग) छः
(घ) सात
14. राज्यों के कार्यों का कौन-सा सिद्धान्त नागरिक की स्वतन्त्रता पर आधारित है? [2007, 08]
(क) आदर्शवाद
(ख) व्यक्तिवाद
(ग) साम्यवाद
(घ) फासीवाद
15. राज्य को अनिवार्य कार्य नहीं है- [2014]
(क) बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना
(ख) मुद्रा का प्रबन्ध करना।
(ग) मनोरंजन की व्यवस्था करना
(घ) कर संग्रह करना
16. निम्नलिखित में से किस सिद्धान्त के अनुसार राज्य शोषण का यन्त्र है? [2014]
(क) व्यक्तिवाद
(ख) आदर्शवाद
(ग) साम्यवाद
(घ) फासीवाद
17. ‘ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स’ नामक पुस्तक के लेखक थे
(क) प्लेटो
(ख) हैरल्ड लॉस्की
(ग) ऐंजिल्स
(घ) कार्ल मार्क्स
18. निम्नांकित में से कौन-सा कल्याणकारी राज्य है?
(क) पाकिस्तान
(ख) चीन
(ग) ब्रिटेन
(घ) मोरक्को
उत्तर
- (ग) फ्रीमैन का,
- (ख) हीगल,
- (ग) 8,
- (ख) जे०एस० मिल,
- (ख) हरबर्ट स्पेन्सर,
- (ख) कौटिल्य का,
- (ख) कार्ल माक्र्स,
- (ख) अराजकतावाद,
- (ग) व्यक्तिवादी,
- (ग) व्यक्तिवाद,
- (ग) कौटिल्य,
- (घ) डॉ० बी०आर० अम्बेडकर,
- (घ) सात,
- (ख) व्यक्तिवाद,
- (ग) मनोरंजन की व्यवस्था करना,
- (घ) फासीवाद,
- (ख) हैरल्ड लॉस्की,
- (ग) ब्रिटेन।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 2 Theories of the Functions of the State (राज्य के कार्यों के सिद्धान्त), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
![]() ] को लघु और दीर्घ वर्ण ( आ, ई, ऊ, अनुस्वार (.), विसर्ग (:)] को गुरु कहते हैं। इनके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण से पूर्व का और हलन्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। हलन्त वर्ण की गणना नहीं की जाती। कभी-कभी लय में पढ़ने पर गुरु वर्ण भी लघु ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उसे लघु ही माना जाता है। कभी-कभी पाद की पूर्ति के लिए अन्त के वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। लघु वर्ण का चिह्न खड़ी रेखा I’ और दीर्घ वर्ण का चिह्न अवग्रह ‘δ’ होता है।
] को लघु और दीर्घ वर्ण ( आ, ई, ऊ, अनुस्वार (.), विसर्ग (:)] को गुरु कहते हैं। इनके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण से पूर्व का और हलन्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। हलन्त वर्ण की गणना नहीं की जाती। कभी-कभी लय में पढ़ने पर गुरु वर्ण भी लघु ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उसे लघु ही माना जाता है। कभी-कभी पाद की पूर्ति के लिए अन्त के वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। लघु वर्ण का चिह्न खड़ी रेखा I’ और दीर्घ वर्ण का चिह्न अवग्रह ‘δ’ होता है।