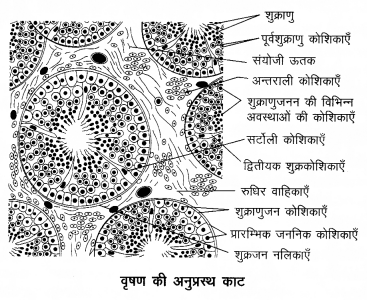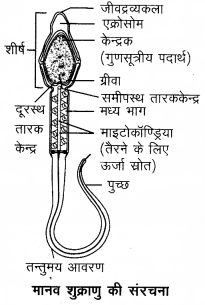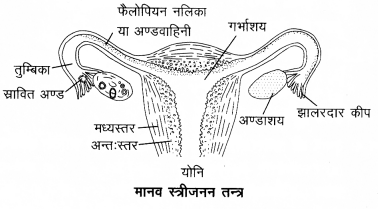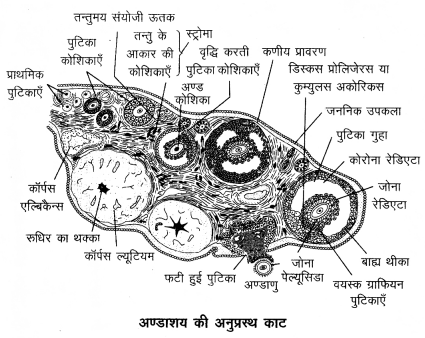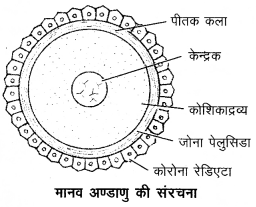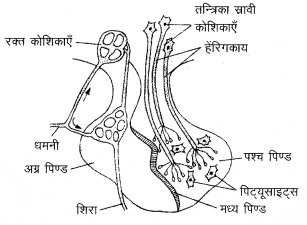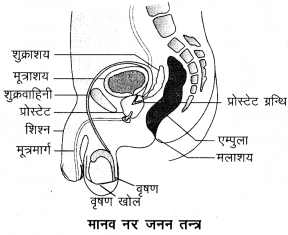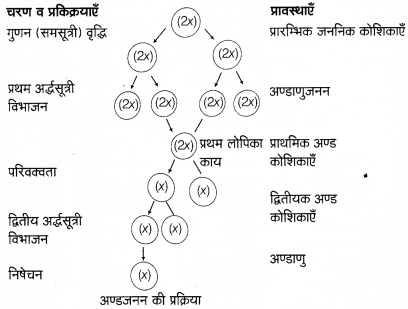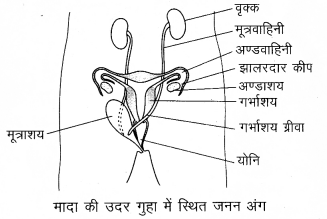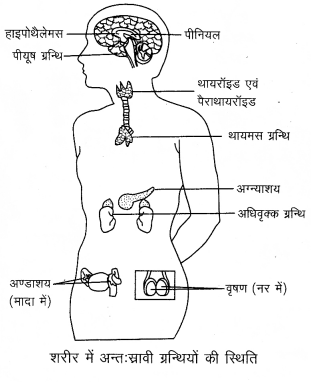UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 3 रश्मिरथी part of UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 3 रश्मिरथी.
| Board |
UP Board |
| Textbook |
SCERT, UP |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Sahityik Hindi |
| Chapter |
Chapter 3 |
| Chapter Name |
रश्मिरथी |
| Number of Questions Solved |
6 |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 3 रश्मिरथी
कथावस्तु पर आधारित प्रश्न
प्रश्न 1.
“रश्मिरथी’ के कथानक में ऐतिहासिकता और धार्मिकता दोनों हैं।” इस कथन के आधार पर इस खंडकाव्य की विशेषताएँ लिखिए। (2018)
अथवा
“रश्मिरथी’ खण्डकाव्य में उदान्त मानव मूल्यों का उदघाटन हुआ है।” स्पष्ट कीजिए। (2018)
अथवा
रश्मिरथी खण्डकाव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। (2018)
अथवा
रश्मिरथी काव्य की कथावस्तु/कथासार अपने शब्दों में लिखिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की कथावस्तु /कथासार (विषय-वस्तु) संक्षेप में लिखिए। (2018, 16, 12, 11)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। (2018, 17, 14)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के कथानक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (2014)
अथवा
‘रश्मिरथी’ के कथानक में ऐतिहासिकता और धार्मिकता दोनों हैं। तर्कसहित उत्तर दीजिए। (2014)
अथवा
रश्मिथी खण्डकाव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। (2016)
उत्तर:
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य रामधारी सिंह ‘दिनकर’ द्वारा रचित है। सर्गानुसार संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है।
प्रथम सर्ग : कर्ण का शौर्य प्रदर्शन
कर्ण का जन्म कुन्ती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुन्ती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे सूत (सारथि) ने बचाया और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर उसका पालन-पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महान् धनुर्धर, शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पाण्डव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया।
सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, किन्तु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वन्द्वयुद्ध के लिए ललकारा। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। इस पर कर्ण ने स्वयं को सूत-पुत्र बताया, तब निम्न जाति का कहकर उसका अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वन्द्वयुद्ध करने के अयोग्य समझा गया, परन्तु दुर्योधन कर्ण की वीरता एवं तेजस्विता से अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र बना लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिन्तित हो उठे और कुन्ती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास हुई।
द्वितीय सर्ग: आश्रमवास
रश्मिरथी खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। (2018, 17, 16)
राजपुत्रों के विरोध से दु:खी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता-चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा, और शान्त रहा। क्योकि कहीं गुरुदेव को निद्रा में विघ्न न पड़ जाए। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव को निद्रा भंग हो गई। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर सन्देह हुआ। अन्त में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श कर वहाँ से चला आया।
तृतीय सर्ग : कृष्ण सन्देश (2017, 15)
बारह वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पाण्डव अपने नगर इन्द्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस माँगते हैं, लेकिन दुर्योधन पाण्डवों को एक सूई की नोंक के बराबर भूमि देने से भी मना कर देता है। श्रीकृष्ण सन्धि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास आते हैं। दुर्योधन इस सन्धि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता और श्रीकृष्ण को ही बन्दी बनाने का प्रयास करता है। श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे भयभीत कर दिया। दुर्योधन के न मानने पर श्रीकृष्ण ने कर्ण को समझाया। श्रीकृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पाण्डवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाए, लेकिन कर्ण ने श्रीकृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा कि वह युद्ध में पाण्डवों की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है, वह उसका आभारी है।
चतुर्थ सर्ग : कर्ण के महादान की कथा
‘रश्मिरथी’ खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। (2008, 12)
जय कर्ण ने पाण्डवों के पक्ष में जाने से मना कर दिया, तो इन्द्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। वह कर्ण को दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इन्द्र के इस छल-प्रपंच को पहचान गया, परन्तु फिर भी उसने इन्द्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुण्डल दान में दे दिए। इन्द्र कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यन्त लज्जित हुए। उन्होंने स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी कहा तथा प्रसन्न होकर कर्ण को ‘एकनी’ नामक अमोघ शक्ति प्रदान की।
पंचम सर्ग : माता की विनती (2013 10)
अथवा
‘रश्मिरथी’ के आधार पर कुन्ती-कर्ण के संवाद की घटना का सारांश लिखिए। (2018)
अथवा
‘रश्मिरथी’ के पंचम सर्ग की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के पंचम सर्ग में कुन्ती और कर्ण के संवाद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। (2010)
कुन्ती को चिन्ता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इससे चिन्तित हो वह कर्ण के पास जाती है और उसे उसके जन्म के विषय में सब बताती है। कर्ण कुन्ती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, किन्तु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पाण्डव को न मारने का वचन कुन्ती को दे देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में पाँच पाण्डवों की माता बनी रहोगी। कुन्ती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कुन्ती की सेवा करने की बात कही। कुन्ती निराश मन से लौट आती है।
षष्ठ सर्ग : शक्ति परीक्षण
श्रीकृष्ण इस बात से भली-भाँति परिचित थे कि कर्ण के पास इन्द्र द्वारा दी गई ‘एकघ्नी शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्रीकृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया।
दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एकनी शक्ति से मार दिया। इस, विजय से कर्ण अत्यन्त दुःखी हुए, पर पाण्डव अत्यन्त प्रसन्न हुए। श्रीकृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघशक्ति से बचा लिया था, परन्तु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया।
सप्तम सर्ग : कर्ण के बलिदान की कथा (2011)
रश्मिरथी खण्डकाव्य के सप्तम सर्ग की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के अन्तिम सर्ग की विवेचना कीजिए। (2014, 13)
कर्ण को पाण्डवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पाण्डवों को पराजित कर देता है, पर माता कुन्ती को दिए गए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ देता है। कर्ण और अर्जुन आमने-सामने हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। एक बार तो वह मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है, तभी श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं।
श्रीकृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता है। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर।
प्रश्न 2.
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (2018)
अथवा
‘रश्मिरथी’ में प्राचीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। स्पष्ट कीजिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ की भाषा की स्वाभाविक सहजता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। (2012)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की विशेषताएँ लिखिए। (2017)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (2014, 13)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। (2013)
अथवा
किन विशेषताओं के आधार पर ‘रश्मिरथी’ को उच्च कोटि का काव्य माना जाता है? (2013)
अथवा
“रश्मिरथी’ काव्य खण्ड में व्यक्ति की उदात्त एवं आदर्श भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। (2011)
अथवा
‘रश्मिरथी में कवि का मन्तव्य कर्ण के चरित्र के शीलपक्ष, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण करना है।” सिद्ध कीजिए। (2014, 11)
उत्तर:
राष्ट्रकवि रामधारीसिंह ‘दिनकर’ सदैव देशप्रेम एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। रश्मिरथी’ खण्डकाव्य इसका अपवाद नहीं है। इस खण्डकाव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
कथानक
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य का कथानक ‘महाभारत’ के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन प्रसंग पर आधारित हैं। इन प्रसंगों ने कर्ण के व्यक्तित्व को एक नई छवि प्रदान की है। कथानक का संगठन सुनियोजित प्रकार से किया गया है।
प्रसंगों का समय भिन्न-भिन्न है, लेकिन उन्हें इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध किया गया हैं। कि कथा के प्रवाह में बाधा नहीं पड़ती और उसका क्रमबद्ध विकास होता है। कथा का अन्त इस प्रकार किया गया है कि वह कर्ण की विशेषताओं को विभूषित करते हुए समाप्त हो जाती है।
पात्र एवं चरित्र-चित्रण
इस खण्डकाव्य में कर्ण के उपेक्षित जीवन और उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर ही प्रकाश डालना कवि का उद्देश्य रहा है। अन्य पात्रों का चुनाव इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है।
कथानक में एक भी अनावश्यक पात्र को स्थान नहीं दिया गया है। कर्ण के चरित्र में वर्तमान युग के सामाजिक स्तर पर उपेक्षित व्यक्तियों एवं कुन्ती के रूप में समाज के नियमों से प्रताड़ित नारियों की व्यथा को स्वर दिया गया है। इस प्रकार इस खण्डकाव्य में पात्रों का चरित्र-चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से हुआ है।
कर्ण जैसे महान् गुणों से सम्पन्न. नायक को कवि ने मुख्य पात्र बनाया है। अन्य पात्रों का चित्रण कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित करने के लिए किया गया है। सम्पूर्ण काव्य में वीर रस को ही प्रधानता दी गई है। छन्दों में अवश्य विभिन्नता है। आदर्शोन्मुख उद्देश्य के लिए लिखी गई इस रचना को सफल खण्डकाव्ये कहा जा सकता हैं।
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य का उद्देश्य (2013)
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के माध्यम से कवि ने उपेक्षित, लेकिन प्रतिभावान मनुष्यों के स्वर को वाणी दी है। यदि कर्ण को बचपन से समुचित सम्मान प्राप्त हुआ होता, जन्म, जाति और कुल आदि के नाम पर उसे अपमानित न किया गया होता तो वह कौरवों का साथ कभी भी नहीं देता। शायद तब महाभारत का युद्ध भी नहीं हुआ होता। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिभाएँ कुण्ठित होकर समाज को पतन की ओर अग्रसर कर देती हैं।
इस खण्डकाव्य में प्राचीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। इसमें समाज में नारियों की मनोदशा का भी यथार्थ वर्णन किया गया है, साथ ही समाज में उनकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रकारे उद्देश्य की दृष्टि से भी यह एक सफल खण्डकाव्य है।
इस खण्डकाव्य में प्राचीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। इसमें समाज में नारियों की मनोदशा का भी यथार्थ वर्णन किया गया है, साथ ही समाज में उनकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रकारे उद्देश्य की दृष्टि से भी यह एक सफल खण्डकाव्य है।
काव्यगत विशेषताएँ
प्रस्तुत खण्डकाव्य ‘रश्मिरथी’ की काव्यगत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
भावपक्षीय विशेषताएँ
1. वण्र्य विषय खण्डकाव्य की दृष्टि से यह एक सफल खण्डकाव्य है। इसके कथानक की रचना में कवि ने अपनी सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया है। दिनकर जी की इस रचना का प्रमुख पात्र कर्ण है। वह समाज के उन व्यक्तियों का प्रतीक है, जो वर्ण-व्यवस्था पर आधारित अमानवीय क्रूरता एवं जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिका के शिकार हैं।
वर्ण व्यवस्था, जाति-प्रथा, एवं ऊँच-नीच की भावना वर्तमान युग की ज्वलन्त समस्याएँ हैं। इन्हीं के कारण भारतीय समाज में योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की उपेक्षा एक सामान्य बात है। कर्ण ऐसे ही पीड़ित एवं उपेक्षित जनों को आदर्श प्रतीक है।
2. प्रकृति चित्रण यद्यपि रश्मिरथी काव्य में प्रकृति चित्रण कवि का विषय नहीं है, तथापि पात्रों के चित्रण-वर्णन के दौरान यत्र-तत्र प्रकृति का चित्रण हुआ है, जो अत्यन्त सशक्त है; जैसे|
- अम्बुधि में आकटक निमज्जित, कनक खचित पर्वत-सा।
- हँसती थीं रश्मियाँ रजत से भरकर वारि विमले को।।
- कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था।
3. रस निरूपण प्रस्तुत खण्डकाव्य में वीर रस की प्रधानता है। साथ ही करुण एवं वात्सल्य रस को भी स्थान दिया गया है। जहाँ कर्ण और कुन्ती का वार्तालाप हैं, वहाँ वात्सल्य रस देखने को मिलता है-
“मेरे ही सुत मेरे सुत को ही मारें,
हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें।’
कलापक्षीय विशेषताएँ। (2010)
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य की कलापक्षीय विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं।
- भाषा-शैली रश्मिरथी खण्डकाव्य में अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग दृष्टिगत होता है। वास्तव में, यह काव्य शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में रचित काव्य है। कवि ने अपनी काव्यात्मक भाषा को कहीं भी बोझिल नहीं होने दिया है। सूक्तिपरकता का भी प्रयोग किया गया है। प्राचीन शब्दावली का प्रयोग किया है, जहाँ युद्ध, घटनाओं एवं परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप देने का प्रयास किया गया है।
- छन्द एवं अलंकार कवि ने प्रत्येक सर्ग में अलग-अलग छन्द प्रयोग किए हैं। विषय, मानसिक परिस्थितियों तथा घटनाओं के संवेदनात्मक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए इनका आयोजन किया गया है। अलंकारों में सहजता और संक्षिप्तता है, वे स्वाभाविक रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः अलंकारों के प्रदर्शन के प्रति कवि की रुचि नहीं है। इस प्रकार भावात्मक एवं कलात्मक दृष्टि से रश्मिरथी’ खण्डकाव्य एक उत्कृष्ट रचना है। यह रचना वर्तमान युग के लिए अत्यन्त उपयोगी है, जो आधुनिक युग के
समाज की बुराइयों को दूर करने का सन्देश देती है।
- उद्देश्य ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के माध्यम से कवि ने उपेक्षित, लेकिन प्रतिभावान मनुष्यों के स्वर को वाणी दी है। यदि कर्ण को बचपन से समुचित सम्मान प्राप्त हुआ होता तथा जन्म, जाति और कुल आदि के नाम पर उसे अपमानित न किया गया होता, तो वह कौरवों का साथ कभी भी नहीं देता। शायद तब महाभारत का युद्ध भी नहीं हुआ होता। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिभाएँ कुण्ठित होकर समाज को पतन की ओर अग्रसर कर देती हैं।
प्रश्न 3.
“रश्मिरथी’ के प्रत्येक सर्ग में संवादात्मक स्थल ही सबसे प्रमुख है।” इस कथन की पुष्टि कीजिए। (2011)
अथवा
“रश्मिरथी खण्डकाव्य की संवाद योजना बड़ी सशक्त है।” इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। (2012)
उत्तर:
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के संवादों में नाटकीयता के गुण विद्यमान हैं। यह नाटकीयता सर्वत्र देखी जा सकती है। इसमें सरलता, सुबोधता, स्वाभाविकता के साथ-साथ प्रभावशीलता भी देखने को मिलती है|
“उड़ती वितर्क-धागे पर चंग-सरीखी,
सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी।
आशा-अभिलाषा भरी, डरी, भरमाई,
कुन्ती ज्यों-ज्यों जाह्नवी तीर पर आई।
कवि ने प्रभावशाली संवाद शैली का अनुसरण करते हुए वर्णनात्मक शैली की कमियों का निराकरण कर दिया है-
“पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरवसेना का शोक गया।
आशा की नवल तरंग उठी, जन-जन में नई उमंग उठी।”
सर्गों का क्रम भी कवि की रचनात्मक विशेषताओं को व्यक्त करता है। छन्द एवं अलंकार कवि ने प्रत्येक सर्ग में अलग-अलग छन्द प्रयोग किए हैं। विषय, मानसिक परिस्थितियों तथा घटनाओं के संवेदनात्मक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए इनका आयोजन किया गया हैं। अलंकारों में सहजता और संक्षिप्तता हैं, वे स्वाभाविक रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः अलंकारों के प्रदर्शन के प्रति कवि की रुचि नहीं हैं। इस प्रकार भावात्मक एवं कलात्मक दृष्टि से ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य एक उत्कृष्ट रचना है। यह रचना वर्तमान युग के लिए अत्यन्त उपयोगी है, जो आधुनिक युग के समाज की बुराइयों को दूर करने का सन्देश देती है।
चरित्र-चित्रण पर आधारित प्रश्न
प्रश्न 4.
“कर्ण महान् योद्धा के साथ-साथ दानवीर भी है।” इस कथन के आधार पर कर्ण का चरित्र-चित्रण कीजिए। (2018)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के नायक के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (2018)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र की चरित्रिक विशेषताओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। (2018)
अथवा
रश्मिरथी के माध्यम से कवि दिनकर ने महारथी कर्ण के किन गुणों पर प्रकाश डाला है? अपने शब्दों में लिखिए। (2017)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएँ बताइट।
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र-चित्रण कीजिए। (2017)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। (2018, 16)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
अथवा
‘रश्मिरथी’ के कर्ण के व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र (नायक कर्ण) का चरित्र-चित्रण (चरित्रांकन/चारित्रिक मूल्यांकन) कीजिए। (2018, 17, 15, 14, 13, 12, 11)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के कर्ण दानवीर थे, परन्तु वह मानसिक अन्तर्द्वन्द्व से भी ग्रस्त थे। ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। (2011)
अथवा
कर्ण के चरित्र में ऐसे कौन-से गुण हैं, जो उसे महामानव की कोटि तक उठा देते हैं? (2012, 11)
अथवा
“रश्मिरथी खण्डकाव्य में उदात्त मानवीय चरित्र का उद्घाटन किया गया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। (2013)
उत्तर:
प्रस्तुत खण्डकाव्य ‘रश्मिरथी’ के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
1. महान् धनुर्धर कर्ण की माता कुन्ती और पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुन्ती अपने पुत्र को नदी में बहा देती है, तब एक सूत उसका लालन-पालन करता है। सूत के घर पलकर भी कर्ण महादानी एवं महान् धनुर्धर बनता है। एक दिन अर्जुन रंगभूमि में अपनी बाणविद्या का प्रदर्शन करता है, तभी वहाँ आकर कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करता है। कर्ण के इस प्रभावपूर्ण प्रदर्शन को देखकर द्रोणाचार्य एवं पाण्डव उदास हो जाते हैं।
2. सामाजिक विडम्बना का शिकार कर्ण क्षत्रिय कुल से सम्बन्धित था, लेकिन उसका पालन-पोषण एक सूत के द्वारा हुआ, जिस कारण वह सूतपुत्र कहलाया और इसी कारण उसे पग-पग पर अपमान का बूंट पीना पड़ा। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर वह अर्जुन को ललकारता है, तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ पर कर्ण को कृपाचार्य की कूटनीतियों का शिकार होना पड़ता है। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे अपमानित होना पड़ा था।
3. सच्चा मित्र कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंगदेश का राजा बना देता है। इस उपकार के बदले भावविह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन जाता है। वह श्रीकृष्ण और कुन्ती के प्रलोभनों को ठुकरा देता है। वह श्रीकृष्ण से कहता है कि मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने ही दिया। अतः मेरा तो रोम-रोम दुर्योधन का ऋणी है। वह तो सब कुछ दुर्योधन पर न्योछावर करने को तत्पर रहता है।
4. गुरुभक्त कर्ण सच्चा गुरुभक्त हैं। वह अपने गुरु के प्रति विनयी एवं श्रद्धालु है। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे तभी एक कीट कर्ण की जंघा में घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, वह चुपचाप पीड़ा को सहता है, क्योकि पैर हिलाने से गुरु की नींद खुल सकती थी, लेकिन आँखें खुलने पर वह गुरु को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। गुरु क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, लेकिन वह अपनी विनय नहीं छोड़ता और गुरु के चरण स्पर्श कर वहाँ से चल देता है।
5. महादानी कर्ण महादानी है। प्रतिदिन प्रात:काल सन्ध्या वन्दना करने के पश्चात् वह याचकों को दान देता है। उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटा। कर्ण की दानशीलता का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है।
“रवि पूजन के समय सामने, जो भी याचक आता था,
मुँह माँगा वह दान कर्ण से, अनायास ही पाता था।”
इन्द्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आते हैं। यद्यपि कर्ण इन्द्र के छल को पहचान लेता है तथापि वह इन्द्र को सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुण्डल दान में दे देता है।
6. महान् सेनानी कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्धभूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पाण्डवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। श्रीकृष्ण भी उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। भीष्म उसके विषय में कहते हैं
“अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे,
तुम मिले कौरवों को वैसे।”
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र दिव्य एवं उच्च संस्कारों से युक्त है। वह शक्ति का स्रोत है, सच्चा मित्र है, महादानी और त्यागी है। वस्तुतः उसकी यही विशेषताएँ उसे खण्डकाव्य का महान् नायक बना देती हैं।
प्रश्न 5.
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर श्रीकृष्ण का चरित्रांकन कीजिए। (2018, 17, 10)
अथवा
‘रश्मिरथी’ के आधार पर श्रीकृष्ण के विराट व्यक्तित्व को संक्षेप में लिखिए।
उत्तर:
‘दिनकर’ जी द्वारा रचित ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर श्रीकृष्ण की चारित्रिक विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं।
1. युद्ध विरोधी एवं मानवता का पक्षधर ‘रश्मिरथी’ के श्रीकृष्ण युद्ध के प्रबल विरोधी हैं और मानवता के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि युद्ध की विभीषिका मानवता के लिए कितनी दुखदायी होती है। पाण्डवों के वनवास से लौटने के पश्चात् श्रीकृष्ण कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न करते हैं, किन्तु हठी दुर्योधन नहीं मानता। कौरवों से पाण्डवों के लिए वे पाँच गाँव ही माँगते हैं। दुर्योधन के द्वारा अस्वीकार करने पर वे सोचते हैं कि वह कर्ण की शक्ति प्राप्त कर ही युद्ध में अपनी जीत की कल्पना कर रहा है। यदि कर्ण उसका साथ छोड़ दे तो यह युद्ध रोका जा सकता है। इस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने कर्ण से कहा-
यह मुकुट मान सिंहासन ले,
बस एक भीख मुझको दे दे।
कौरव को तेज रण रोक सखे,
भु का हर भावी शोक सखे।
2. निडर एवं स्फुटवक्ता श्रीकृष्ण निडर एवं स्फुटवक्ता अर्थात् बात को स्पष्ट कहने वाले हैं। वे युद्ध नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कौरवों और पाण्डवों के मध्य सुलह हो जाए। इसके आधार पर उन्हें कायर नहीं कहा जा सकता। वे दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन जब वह उनके हित की दृष्टि से दी गई सलाह को नहीं मानती है तो वे कहते हैं कि-
तो ले अब मैं भी जाता है,
अन्तिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन-जय या कि मरण होगा।
3. सदाचारी एवं व्यावहारिक श्रीकृष्ण सदाचारी एवं व्यावहारिक हैं। उनके सभी कार्य सदाचार एवं शील के परिचायक हैं। उनका उद्देश्य सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना है और वे यही चाहते हैं कि सभी सदाचरण करें। वे सदाचार को ही जीवन का सार मानते हुए कहते हैं कि-
नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है,
विभा का सार शील पुनीत में है।
4. गुणवानों के पक्षधर ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के श्रीकृष्ण गुणवान व्यक्तियों के प्रबल समर्थक एवं प्रशंसक हैं। इस कारण वे अपने विरोधी के गुणों का भी सम्मान करते हैं। यद्यपि कर्ण कौरव पक्ष का योद्धा था फिर भी श्रीकण के मन में उसके गुणों के प्रति बहुत आदर है। वे उसका गुणगान करते नहीं थकते। उसकी मृत्यु के उपरान्त वे अर्जुन से उसके बारे में कहते हैं कि-
मगर, जो हो, मनुज सुवरिष्ठ था वह,
घनुर्धर ही नहीं, घमिष्ठ था वह।
वीर शत बार धन्य
तुझ-सा न मित्र कोई अनन्य।
5. कूटनीतिज्ञ ‘दिनकर’ द्वारा रचित ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के श्रीकृष्ण कूटनीतिज्ञ हैं। महाभारत के श्रीकृष्ण के चरित्र से उनके चरित्र की विशेषताएँ मिलती हैं, किन्तु इस खण्डकाव्य में उनके कूटनीतिज्ञ स्वरूप का ही चित्रण हुआ है। पाण्डवों की जीत का आधार उनकी कूटनीति ही थी। वे पाण्डवों की ओर से कूटनीति की चाल चलकर दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। उनकी कूटनीतिज्ञता का पता इन पंक्तियों में उनके द्वारा कहा गया यह कथन स्पष्ट करता है–
कुन्ती का तू ही तनय श्रेष्ठ,
बलशील में परम श्रेष्ठ।
मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम,
तेरा अभिषेक करेंगे हम,
6. अलौकिक गुणों से युक्त ‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के श्रीकृष्ण महाभारत के श्रीकृष्ण की ही तरह अलौकिक गुणों से युक्त हैं। वे लीलामय पुरुष हैं, क्योंकि उनमें अलौकिक शक्ति विद्यमान है। जब वे दुर्योधन के दरबार में पाण्डवों के दूत बनकर जाते हैं, तो दुर्योधन उन्हें बाँधना चाहता है और कैद करना चाहता है, तो उस समय वे अपना लीलामय विराट स्वरूप दिखाते है-
हरि ने भीषण हुँकार किया,
अपना स्वरूप विस्तार किया,
डगमग-इगमग दिग्गज डोले,
भगवान, कुपित होकर बोले
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे,
हाँ, हाँ दुर्योधन! बाँध मुझे।
इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं कि श्रीकृष्ण निडर एवं स्फुटवक्ता, अलौकिक गुणों से युक्त होते हुए महाभारत के श्रीकृष्ण के चरित्र के समस्त गुणों को अपने अन्दर समाहित किए हुए हैं। इसके साथ-ही-साथ उनका चरित्र लोकमंगल की भावना से युक्त है। श्रीकृष्ण का यह स्वरूप कवि ने इस खण्डकाव्य में युग के अनुसार ही प्रकट किया है। इसके कारण उनके महाभारतकालीन चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है-
प्रश्न 6.
“रश्मिरथी खण्डकाव्य के नारी-पात्र कुन्ती के चरित्र में कवि ने मातृत्व के भीषण अन्तर्द्वन्द्व की पुष्टि की है।” इस कथन की सार्थकता कीजिए। (2018)
अथवा
‘रश्मिरथी’ के आधार पर कुन्ती के चरित्र की विशेषताएँ बताइए। (2016)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के प्रधान नारी (कुन्ती) पात्र का चरित्रांकन कीजिए। (2018, 16)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य के आधार पर कुन्ती के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। (2013, 12, 11)
अथवा
“कुन्ती के चरित्र में कवि ने मातृत्व के भीषण अन्तर्द्वन्द्व की सृष्टि की है।” इस कथन के आधार पर कुन्ती का चरित्र-चित्रण कीजिए। (2010)
अथवा
‘रश्मिरथी’ खण्डकाव्य में प्रस्तुत कुन्ती के मन की घुटन का विवेचन कीजिए। (2011)
उत्तर:
कुन्ती पाण्डवों की माता है। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कुन्ती के गर्भ से ही हुआ था। इस प्रकार कुन्ती के पाँच नहीं वरन् छः पुत्र थे। कुन्ती की चारित्रिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं।
- समाज भीरू कुन्ती लोकलाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती है। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसे युवा और धीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती। जब युद्ध की विभीषिका सामने आती है, तो वह कर्ण से एकान्त में मिलती है और अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करती है।
- एक ममतामयी माँ कुन्ती ममता की साक्षात् मूर्ति है। कुन्ती को जब पता चलता है कि कर्ण का उनके अन्य पाँच पुत्रों से युद्ध होने वाला है, तो वह कर्ण को मनाने उसके पास जाती है और उसके प्रति अपना ममत्व एवं वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है। वह नहीं चाहती कि उनके पुत्र युद्धभूमि में एक-दूसरे के साथ संघर्ष करें। यद्यपि कर्ण उनकी बातें स्वीकार नहीं करता, पर वह उसे आशीर्वाद देती है, उसे अंक में भरकर अपनी वात्सल्य भावना को सन्तुष्ट करती है।
- अन्तर्द्वन्द्व ग्रस्त कुन्ती के पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए थे, तब कुन्ती के मन में भीषण अन्तर्द्वन्द्व मचा हुआ था, वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी कि पाँचों पाण्डवों और कर्ण में से किसी की भी हानि हो, पर वह हानि तो मेरी ही होगी। वह इस स्थिति को रोकना चाहती थीं, परन्तु कर्ण के अस्वीकार कर देने पर वह इस नियति को सहने के लिए विवश हो जाती है। इस प्रकार कवि ने ‘रश्मिरथी’ में कुन्ती के चरित्र में अनेक उच्च गुणों का समावेश किया है। और इस विवश माँ की ममता को महान् बना दिया है।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 3 रश्मिरथी help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Sahityik Hindi खण्डकाव्य Chapter 3 रश्मिरथी, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.