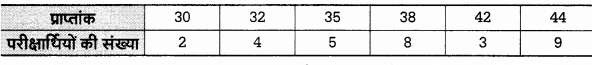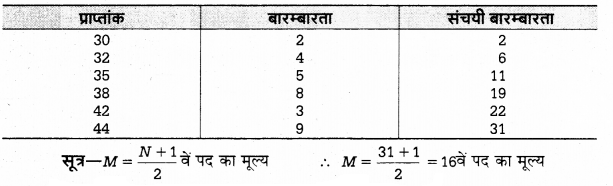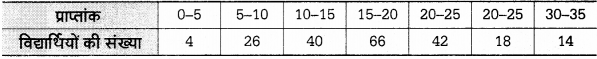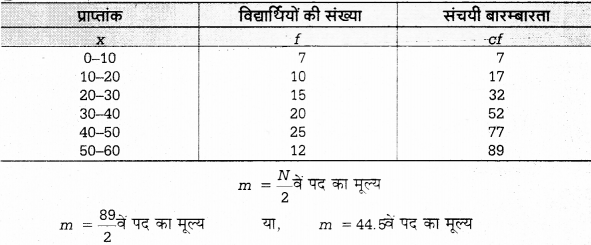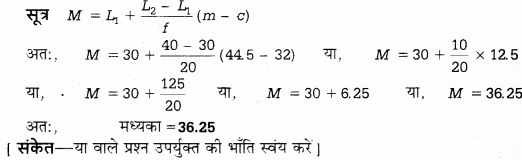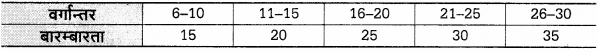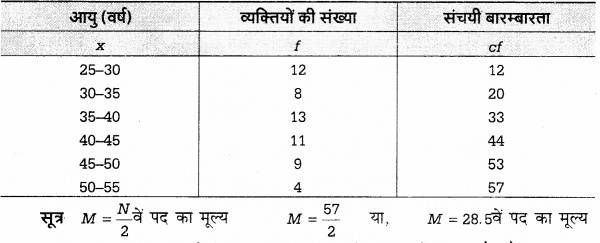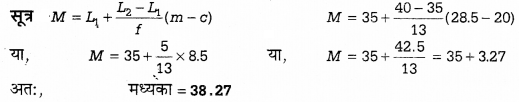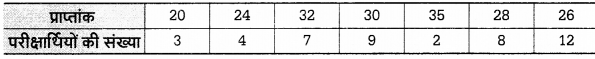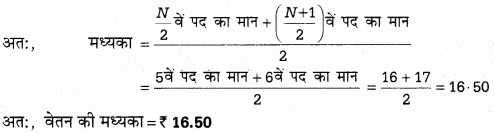UP Board Solutions for Class 12 Civics संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत are part of UP Board Solutions for Class 12 Civics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Civics संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत.
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Civics |
| Chapter | 22 b |
| Chapter Name | संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत |
| Number of Questions Solved | 39 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Civics संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (6 अंक)
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। उनमें से सुरक्षा परिषद् के संगठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। [2007, 11]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या लिखिए। [2013]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए तथा विश्व शान्ति की स्थापना में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। [2013]
उतर :
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ‘सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन के आधार पर 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र के छः मुख्य अंग हैं, जो निम्नलिखित हैं –
1. साधारण सभा या महासभा – साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। संघ के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य को इसमें 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है।
2. सुरक्षा परिषद् – यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है। इसका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 1 जनवरी, 1966 से परिषद् में 15 सदस्य हैं जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ‘हृदय’ व ‘दुनिया की पुलिसमैन’ कही जाने वाली सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद् में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य व 10 अस्थायी सदस्य हैं। पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा दो वर्षों के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद् में किसी भी विषय पर निर्णय 15 में से 9 सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति द्वारा होता है। इसमें भी 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों का स्वीकारात्मक मत होना अनिवार्य होता है। यदि पाँचों में से एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव पर विरोध प्रकट करता है तो प्रस्ताव को रद्द समझा जाता है। इस अधिकार को स्थायी राष्ट्रों का निषेधाधिकार (वीटो) कहा जाता है।
3. आर्थिक व सामाजिक परिषद् – इस परिषद् का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्राप्त करना है। इसमें इस समय 54 सदस्य हैं।
4. प्रन्यास परिषद् – इस परिषद् का मुख्य कार्य अविकसित और पिछड़े हुए प्रदेशों के हितों की रक्षा करना है। यह कार्य उन्नत व विकसित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय – यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो साधारण सभा व सुरक्षा परिषद् द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से होते हैं। न्यायालय केवल ऐसे ही विवादों पर विचार कर सकता है जिनसे सम्बन्धित सभी पक्ष विवादों को न्यायालय के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करें।
6. सचिवालय – इसके सचिवालय का प्रधान महामन्त्री और संघ की आवश्यकतानुसार कर्मचारी वर्ग होता है। महामन्त्री की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है।
सुरक्षा परिषद् के कार्य
संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र की धारा 24, 25 व 26 के अन्तर्गत उल्लिखित सुरक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –
- विश्व-शान्ति व सुरक्षा बनाये रखना तथा इसके भंग होने की स्थिति में कारणों की जाँच करना व विचार-विमर्श कर समझौता, अपील या बाध्यकारी आदेश देकर उसका समाधान करना।
- किसी राष्ट्र द्वारा निर्णय व नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही (कूटनीतिक, आर्थिक या सैनिक) करना।
- महासभा में नये सदस्य राष्ट्रों के आवेदन-पत्रों पर विचार करना व सुझाव देना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सुरक्षा परिषद् को एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करने से सम्बन्धित है।
- विश्व में प्राणघातक अस्त्रों के नियमन का प्रयत्न करना।
[ संकेत – विश्व शान्ति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के अध्ययन हेतु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करें। ]
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता तथा असफलता के कारण उदाहरण सहित बताइए। [2007]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। [2013]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व-शान्ति स्थापित करने में किस प्रकार सहायक है?
या
विश्व शान्ति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र का क्या योगदान है? [2011]
उत्तर :
सन् 1920 में स्थापित राष्ट्र संघ की असफलता के कारण सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से विश्व के राष्ट्रों को यह आशा बँधी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा विवादों का निराकरण शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराकर विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने में पूर्ण सफल होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में अत्यधिक सीमा तक सफल रहा है, परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन महाशक्तियों की स्वार्थपरता के कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में असफल भी रहा है। खाड़ी युद्ध, कुर्द समस्या, रूस का चेचेन्या पर आक्रमण, पूर्वी तिमोर की समस्या, परमाणु शस्त्रों के परिसीमन में अवरोध आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ इस तथ्य की पुष्टि करती हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ (सफलताएँ)
विश्व-शान्ति को बनाये रखने के लिए संघ की सुरक्षा परिषद् तथा महासभा ने निम्नलिखित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में एक बड़ी सीमा तक सफलता प्राप्त की है –
1. रूस-ईरान विवाद (1946 ई०) – संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से ईरान के अजरबैजान क्षेत्र में सोवियत संघ की सेनाओं के द्वारा प्रवेश करने की समस्या को दोनों देशों में सीधी वार्ता कराकर 21 मई, 1946 तक रूसी सेनाओं से ईरानी प्रदेश को खाली करा दिया गया।
2. यूनान विवाद (1946-47 ई०) – 3 दिसम्बर, 1946 को यूनान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से शिकायत की कि उनकी सीमाओं पर साम्यवादी राज्य आक्रामक कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यूनान तथा साम्यवादी राज्यों में समझौता कराकर इस विवाद को सुलझाने में सफलता प्राप्त की।
3. हॉलैण्ड-इण्डोनेशिया विवाद (1947-48 ई०) – द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त 1947 ई० में हॉलैण्ड तथा इण्डोनेशिया के मध्य युद्ध छिड़ गया। 20 जुलाई, 1947 को ऑस्ट्रेलिया तथा भारत ने इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाया। समिति के प्रयत्नों के फलस्वरूप 17 जनवरी, 1948 को दोनों पक्षों में एक अस्थायी समझौता हो गया।
4. बर्लिन का घेरा (1948 ई०) – 23 सितम्बर, 1948 को मित्र-राष्ट्रों ने रूस के द्वारा बर्लिन की घेरेबन्दी का मामला सुरक्षा परिषद् में उठाया। परिणामस्वरूप 4 मई, 1949 के एक समझौते के द्वारा रूस ने 12 मई, 1949 को बर्लिन की घेराबन्दी समाप्त कर दी।
5. फिलिस्तीन की समस्या (1948 ई०) – संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से 13 सितम्बर, 1993 को फिलिस्तीन को सीमित स्वतन्त्रता प्रदान करने वाले एक समझौते पर यासिर अराफात और इजराइली प्रधानमन्त्री रॉबिन ने हस्ताक्षर कर दिये। 25 जुलाई, 1994 को जॉर्डन के शाह हुसैन और रॉबिन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी शत्रुता का अन्तं कर दिया।
6. सीरिया और लेबनान की समस्या (1946 ई०) – 4 फरवरी, 1946 को सीरिया और लेबनान ने अपने प्रदेश से फ्रांसीसी सेनाओं को हटाने की माँग की। सुरक्षा परिषद् में विश्व जनमत के दबाव को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया तथा लेबनान से अपनी सेनाएँ वापस बुला लीं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र इस समस्या को हल करने में सफल रहा।
7. स्पेन की समस्या (1946 ई०) – 1946 ई० में पोलैण्ड ने सुरक्षा परिषद् से यह शिकायत की कि स्पेन में फ्रांको के तानाशाही शासन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की कि फ्रांको की सरकार को संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहायक संस्थाओं की सदस्यता से वंचित कर दिया जाए, किन्तु बाद में यह सिफारिश रद्द कर दी गयी और 1955 ई० में स्पेन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी प्रदान कर दी गयी।
8. कोरिया की समस्या (1950-51 ई०) – द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त कोरिया; उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य विभक्त हो गया था। महाशक्तियों के आपसी मतभेदों के फलस्वरूप 1950 ई० में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर भीषण आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। जुलाई, 1951 ई० में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और युद्ध भी बन्द हो गया। यह संयुक्त राष्ट्र की एक उल्लेखनीय सफलती थी, क्योंकि उसी के प्रयासों के कारण ही कोरिया युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण नहीं कर सका था।
9. कश्मीर समस्या – पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर, 1947 को उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबाइलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। 1 जनवरी, 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद् से इस विषय में शिकायत की। 17 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद् ने दोनों पक्षों को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया, परन्तु युद्ध समाप्त नहीं हुआ। समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित आयोग ने दोनों पक्षों से बातचीत की। पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्षों ने 1 जनवरी, 1949 को युद्ध-विराम मान लिया।
10. स्वेज नहर की समस्या (1956 ई०) – 26 जुलाई, 1956 को कर्नल नासिर द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर मिस्र में स्वेज नहर कम्पनी’ की सम्पत्ति को जब्त (Freeze) कर लिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि डलेस ने यह प्रस्ताव रखा कि स्वेज नहर को निरस्त अधिकार-क्षेत्र में रखा जाए और उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर बोर्ड’ को सौंप दिया जाए जो कि अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष प्रस्तुत करे तथा स्वेज नहर को सभी देशों के लिए खोल दिया जाए। 15 नवम्बर, 1956 को संयुक्त राष्ट्र की सेना की एक टुकड़ी कर्नल नासिर की अनुमति से मिस्र पहुँच गयी। अप्रैल, 1957 ई० में स्वेज नहर पुनः जहाजों के आवागमन के लिए खोल दी गयी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ स्वेज नहर की समस्या को हल करने में सफल हुआ।
11. कांगो की समस्या (1960 ई०) – कांगो की भीषण समस्या को भी हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता प्राप्त हुई। कांगो का एकीकरण करके संयुक्त राष्ट्र ने अपना काम पूरा कर दिया, परन्तु आज भी कांगो की समस्या पूरी तरह सुलझ नहीं पायी है।
12. साइप्रस की समस्या (1964 ई०) – 16 अगस्त, 1960 को साइप्रस ब्रिटिश अधीनता से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र गणराज्य बन गया। तत्पश्चात् साइप्रस में उत्पन्न गृहयुद्ध की समस्या को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वहाँ शान्ति सेना भेजी गयी व सेना द्वारा वहाँ शान्ति स्थापित की गयी।
13. डोमिनिकन गणराज्य विवाद (1965 ई०) – 1964 ई० के अन्त में वेस्टइण्डीज के हेटी टापू के एक भाग में स्थित डोमिनिकन गणराज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिकी राज्यों के प्रयत्नों के कारण दोनों पक्षों में एक समझौते के बाद वहाँ शान्ति स्थापित हो गयी।
14. अरब-इजराइल युद्ध (1967 ई०) – 7 जून, 1967 को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित करके अरबों तथा इजराइल को तत्काल ही युद्ध बन्द करने का आदेश दिया। फलस्वरूप 8 जून, 1967 को दोनों पक्षों ने युद्ध बन्द कर दिया।
15. अरब-इजराइल युद्ध (1973 ई०) – अक्टूबर, 1973 ई० में अरब-इजराईल के बीच पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया। लेकिन महाशक्तियों की स्वार्थप्रियता के कारण तत्काल ही सुरक्षा परिषद् ने इस युद्ध को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की। जब युद्ध उग्र रूप धारण करने लगा तब संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 11 नवम्बर, 1973 को इज़राइल तथा मिस्र के मध्य एक छः सूत्रीय समझौता हो गया।
16. वियतनाम की समस्या (1974 ई०) – 1964 ई० में अमेरिका ने वियतनाम संघर्ष में खुलकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। महाशक्तियों की स्वार्थप्रियता के कारण उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य संघर्ष 1974 ई० तक चलता रहा। विश्व जनमत के दबाव के कारण अमेरिका को वियतनाम से अपनी सेनाएँ हटानी पड़ीं और अन्ततः उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया।
17. दक्षिणी रोडेशिया की समस्या (1980 ई०) – संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप 17 अप्रैल, 1980 को भीषण छापामार युद्ध के पश्चात् रोडेशिया को स्वाधीनता प्राप्त हो गयी और ‘जिम्बाब्वे’ के नाम से उसे संघ की सदस्यता भी दे दी गयी।
18. अमेरिकी बन्धकों की समस्या – 4 नवम्बर, 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास की घेराबन्दी करके कुछ कट्टर इस्लामी छात्रों ने 52 अमेरिकी राजनयिकों को बन्दी बना लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से अमेरिकी बन्धकों को मुक्ति मिल सकी।
19. फाकलैण्ड की समस्या (1982 ई०) – 12 अप्रैल, 1982 को अर्जेण्टाइना की सेनाओं ने अचानक ही फाकलैण्ड द्वीपसमूह पर आक्रमण करके उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से 14 जून, 1982 को अर्जेण्टाइना की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और फाकलैण्ड पर पुन: ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया।
20. ईरान-इराक युद्ध (1988 ई०) – सीमा विवाद को लेकर 22 सितम्बर, 1980 को ईरान व इराक के मध्य उत्पन्न युद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता करने पर अगस्त, 1988 ई० में समाप्त हुआ।
21. नामीबिया की समस्या (1990 ई०) – नामीबिया एक लम्बे समय से अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में 13 दिसम्बर, 1988 को कांगो की राजधानी ब्रांजविले में दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा और अंगोला के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के बाद 21 मार्च, 1990 को नामीबिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया।
22. कुवैत की समस्या (खाड़ी युद्ध 1991 ई०) – इराक ने अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसी देश कुवैत पर अधिकार कर लिया। सुरक्षा परिषद् के आदेश से संयुक्त राज्य अमेरिका व मित्र-राष्ट्रों की सेना ने खाड़ी युद्ध में इराक को नतमस्तक करके कुवैत को मुक्त कराया।
23. यूगोस्लाविया की समस्या (1992 ई०) – 1992 ई० में यूगोस्लाविया में भीषण जातीय संघर्ष छिड़ गया, जिसमें बीस हजार से अधिक लोग मारे गये। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में भारत के लेफ्टीनेण्ट जनरल सतीश नाम्बियार के नेतृत्व में 25 हजार सैनिकों की एक सेना यूगोस्लाविया में शान्ति स्थापना हेतु भेजी गयी। इस सेना ने यूगोस्लाविया (वर्तमान बोसनिया) में शान्ति की स्थापना की।
24. सोमालिया की समस्या (1993 ई०) – 1991 ई० को राष्ट्रपति मोहम्मद सैयद की पदच्युति के बाद गृहयुद्ध और अधिक तेज हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना की सहायता से सोमालिया में शान्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के अनेक राष्ट्रों की गम्भीर समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। यदि इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की सकारात्मक भूमिका नहीं होती तो तीसरे विश्व युद्ध की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकती थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएँ।
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ जटिल समस्याएँ ऐसी भी हैं जिनका समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा है; जैसे –
- कम्पूचिया की समस्या।
- रूस का चेचेन्या पर आक्रमण (1996 ई०)।
- खाड़ी क्षेत्र की समस्या (दिसम्बर, 1996 ई०)।
- अफगानिस्तान में गृहयुद्ध (अक्टूबर, 1996 ई०)।
- कोसोवो की समस्या (1999 ई०) जिसमें NATO संगठन के देशों ने अमेरिका तथा ब्रिटेन के नेतृत्व में कोसोवो पर सैनिक हमला किया।
- इराक के सैनिक ठिकानों की खोज का कार्यक्रम (1998 ई०), जहाँ रासायनिक अस्त्रों के भण्डार को छुपाया गया था। कुछ स्थानों की तलाशी न दिये जाने के कारण अमेरिका ने इराक पर (1999 ई०) सैनिक आक्रमण कर दिया।
- पाकिस्तान (जून, 1999 ई०) द्वारा भारतीय सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन कर भाड़े के घुसपैठियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में युद्ध जैसी कार्यवाही करना।
- 1999 ई० में उत्पन्न पूर्वी तिमोर की समस्या।
- अफगानिस्तान में अकवाद की समस्या (2001 ई०), इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष (मार्च 2002 ई०) तथा अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण (मार्च 2003 ई०), रूस का चेचेन्या में हस्तक्षेप (दिसम्बर 2004 ई०), इराक में आतंकी विस्फोट (अप्रैल 2005 ई०), रूस व जापान के बीच द्वीपों का विवाद (जनवरी 2006 ई०), ईराने की परमाणु नीति (मार्च 2006 ई०) आदि।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, फिर भी हम संयुक्त राष्ट्र को एक आदर्श संस्था के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस संस्था में महाशक्तियों के प्रभुत्व का बोलबाला है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक टिप्पणी की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका ने खरीद लिया है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा विश्व राजनीति पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया है।
प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शान्ति की स्थापना में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। [2007]
या
‘भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदैव ही पूर्ण आस्था रही है। इस कथन के प्रकाश में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका की विववेचना कीजिए।
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शान्ति में भारत की भूमिका
भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र को विश्व-शान्ति स्थापित करने वाला एक आवश्यक उपागम मानता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों तथा विशेष अभिकरणों में सक्रिय भाग लेकर महत्त्वपूर्ण कार्य किये है। भारत ने आज तक संयुक्त राष्ट्र के आदेशों का पूर्णतः पालन किया है। कोरिया तथा हिन्द-चीन में शान्ति स्थापित करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर कांगों में शान्ति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजीं जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित रखा।
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में विश्व शान्ति की स्थापना में भूमिका को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।
1. गैर-राष्ट्रों के संघर्षों की समाप्ति में योगदान – भारत ने क्रोशिया तथा बोस्निया-हर्जेगोविना में हुए संघर्षों को समाप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों को पूरा समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दल के प्रयासों से लेफ्टिनेण्ट जनरल सतीश नाम्बियार की माण्ड में यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन के लिए भेजी गई सेना की विश्वभर में प्रशंसा हुई। भारत ने सोमालियों को मानवीय सहायता तत्काल भेजने में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन किया तथा उसके कार्यों में सहयोग दिया।
2. भारतीय सेनाओं का योगदान – संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेनाओं के कार्यों की प्रशंसा की है। भारत ने कांगो में शान्ति स्थापना के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं। उन्होंने निष्पक्षता के साथ वहाँ शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना करके देश की एकता को बचाया। इसके अतिरिक्त, भारत ने सोमालिया में भी शान्ति स्थापनार्थ अपनी सेवाएँ भेजीं। भारतीय सेनाएँ यूगोस्लाविया, कम्बोडिया, लाइबेरिया, अंगोला तथा मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र की शान्ति स्थापनार्थ कार्यवाही में सफलतापूर्वक भाग लेकर सम्मान सहित स्वदेश लौटी हैं। भारत ने एक टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र अंगोला वेरीफिकेशन मिशन (U.N. Angola Verification Mission) पर जुलाई, 1995 में भेजी। वर्ष 1996-97 की अवधि में लगभग 1,100 भारतीय सैनिक, स्टाफ अधिकारी तथा सैनिक पर्यवेक्षक अंगोला में तैनात रहे। इतना ही नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र रवांडा मिशन पर थल सेना की एक बटालियन भेजी जिसमें 800 सैनिकों की टुकड़ी तथा एक आन्दोलन नियन्त्रण यूनिट सम्मिलित थी। 22 सैन्य पर्यवेक्षक तथा 9 स्टाफ अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया था। इस समय 5 सैनिक पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र इराक-कुवैत पर्यवेक्षक मिशन में और 6 पर्यवेक्षक लाइबेरिया में तैनात हैं।
सम्पूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र की शान्ति मिशन की वर्तमान 17 कार्यवाहियों में इस समय लगभग 80,000 असैनिक तथा सैनिक कार्यरत् हैं, जिनमें भारत के 6,000 कार्मिक हैं।। नवम्बर, 1998 में दक्षिणी लेबनान में भारतीय इन्फैण्ट्री बटालियन के सम्मिलित हो जाने से भारत संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता देने वाला देश बन गया है।
3. आर्थिक सहयोग पर महत्त्वपूर्ण कार्य – भारत ने संयुक्त राष्ट्र से सम्बन्धित देशों के आह्वान पर आर्थिक सहयोग पर अधिक-से-अधिक बल दिया है तथा यथायोग्य सहायता भी प्रदान की है। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थापित संयुक्त । कमीशन तथा तकनीकी कार्यक्रमों के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए तथा प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक सहयोग का समर्थन किया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भारत ने आर्थिक विकास के लिए विश्व में अपनी अच्छी साख बनाई है। विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों . में, अंकटाड की बैठकों में, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं पर होने वाले विशेष विचारविमर्श में, विशेषकर कच्चे माल और विकास के विषय में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्याप्त बल दिया गया है।
4. लोकतन्त्र के सिद्धान्त पर बल – संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श की अवधि में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतान्त्रिक स्वरूप और सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को बढ़ी । हुई सदस्य संख्या के अनुरूप अधिक प्रतिनिधि बनाने का दृढ़ता के साथ समर्थन किया। भारत ने अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत ही लोकतन्त्र के सिद्धान्त को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा 1994 ई० में महासभा के 49वें सत्र में सामान्य बहस के समय परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा भी किया। महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने कहा कि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का आकार, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में भारत को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य होना अनिवार्य समझा जाना चाहिए।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से ही मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगी रहे हैं। भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। विशेषतः संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियों के तत्त्वावधान में एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों को दी गई सहायता तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा में भारत ने पूर्ण सहयोग दिया है। आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त जातियों, समुदायों के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में भारत का योगदान प्रशंसनीय रहा है।
लघु उत्तरीय प्रठा (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संगठनात्मक कमियों पर प्रकाश डालिए तथा उसके सुधार के उपाय सुझाइए। [2007]
उत्तर :
सुरक्षा परिषद् की संगठनात्मक कमियों को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी संरचना पर दृष्टिपात करना वांछित होगा।
सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है और इसका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 1 जनवरी, 1966 से परिषद् में 15 सदस्य हैं जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। परिषद् के 5 स्थायी सदस्य हैं–संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और साम्यवादी चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए होता है। 1965 ई० के संशोधन के अनुसार इन अस्थायी सदस्यों में 5 स्थान अफ्रीकी, एशियाई राज्यों, 2 स्थान लैटिन अमेरिकी राज्यों, 2 स्थान पश्चिमी यूरोपीय देशों और एक स्थान पूर्वी यूरोपीय राज्यों को मिलना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों को परिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए।
संगठनात्मक कमियाँ तथा सुधार के उपाय
सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में यह अनुभव किया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद् में एशियाई-अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अत: परिषद् में अस्थायी और स्थायी विशेषतया स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
सामान्य सुझाव यह है कि परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी जानी चाहिए और जापान, जर्मनी, भारत तथा अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका के एक-एक देश को परिषद् की स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत के निरन्तर सहयोग के आधार पर भारत का परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए ठोस दावा बनता है। जापान ने भी भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान किए जाने का पुरजोर समर्थन किया है।
परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त है। यह अधिकार भी विवादास्पद तथा दोषपूर्ण है। यह भी सुझाव है कि सुरक्षा परिषद् में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किये जाएँ तथा निषेधाधिकार को निरस्त कर दिया जाए।
![]()
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
या
संयुक्त राष्ट्र संघ के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। [2014, 15, 16]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। [2016]
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य
अनुच्छेद 1 में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र का सर्वप्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शान्ति बनाए रखना है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं –
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- पारस्परिक मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना।
- प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार देना।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना।
- समस्त मानव-जाति के अधिकारों का सम्मान करना।
संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त
घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं –
- सभी सदस्य राष्ट्र एकसमान और सम्प्रभुतासम्पन्न हैं।
- सभी सदस्य राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।
- सदस्य-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे।
- सदस्य-राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के प्रतिकूल न तो बल प्रयोग की धमकी देगे और न ही शक्ति का प्रयोग करेंगे।
- सदस्य-राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहायता देंगे और उन राष्ट्रों की सहायता नहीं करेंगे, जिनके विरुद्ध संघ ने कोई कार्यवाही की हो।
- कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की स्थापना व सदस्यता पर संक्षिप्त टिपणी लिखिए।
उतर :
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर विश्व में शान्ति स्थापित करने तथा विश्व शान्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई थी, परन्तु अनेक कारणों से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में असफल रहा और 1939 ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया; अतः भविष्य में युद्धों को रोकने और विश्व में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से युद्धकाल में ही किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई, जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। फलतः युद्धकाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार किया गया और अन्त में इसी सन्दर्भ में मित्र-राष्ट्रों को 26 जून, 1945 को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैनफ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र’ का गठन किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में एक घोषणा-पत्र (Charter) तैयार किया गया। इस घोषणा-पत्र पर 24 अक्टूबर, 1945 को 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान इसका नया सदस्य राष्ट्र है, जिसे 2011 में इसमें शामिल किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।
सदस्यता
विश्व का कोई भी शान्तिप्रिय राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की शर्ते या नियम मानने को तैयार हो, इसको सदस्य बन सकता है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिया जाता है, जिस पर सुरक्षा परिषद् एवं महासभा विचार करती हैं। दोनों की स्वीकृति पाने पर राष्ट्र को सदस्यता–पत्र दे दिया जाता है। सुरक्षा परिषद् बहुमत से सदस्यता प्रदान करती है, परन्तु इसके लिए परिषद् के स्थायी सदस्यों की सहमति तथा महासभा के 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। सदस्यता प्राप्ति के समय उसे (सदस्यता प्राप्त करने वाले देश को) पारस्परिक झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने की स्थिति में उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्यवाही की जाती है।
प्रश्न 4.
संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना कार्यों में भारत की भूमिका बताइए। [2008]
उत्तर :
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। भारत ने इस उद्देश्य की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा सहयोग दिया है। 1947 ई० में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और अगस्त, 1965 ई० में पुनः जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत ने राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को माना, जब कि वह चाहता तो शक्ति के आधार पर इस प्रश्न को सुलझा सकता था।
1950 ई० में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण से ‘कोरियाई युद्ध’ आरम्भ हो गया और ऐसा लगने लगा कि कहीं यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप न ले ले। इस युद्ध को रोकने के लिए ही भारत ने प्रस्ताव पारित कराया। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने वाले आयोग का अध्यक्ष भी भारत को ही बनाया गया। जनरल थिमैया की अध्यक्षता में भारतीय सैनिकों ने युद्ध-बन्दियों को स्वदेश लौटाने का कार्य बड़ी सावधानी से किया।
कोरियों की तरह ही कांगो में भी भारतीय सैनिक भेजे गये तथा प्रतिनिधि श्री राजेश्वर दयाल ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इस समस्या को हल कराने में श्री वी० कृष्णामेनन ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। भारत के प्रयास से ही जेनेवा में सम्मेलन बुलाया गया और यहीं युद्ध-बन्दी तथा अस्थायी सन्धि का प्रस्ताव पास हुआ। युद्धविराम सन्धि को लागू करने के लिए बनाये गये आयोग की अध्यक्ष भी भारत को ही बनाया गया। लाओस और कम्बोडिया में भी भारतीय सेना ने बहुत प्रशंसनीय भूमिका निभायी।
हंगरी एवं स्वेज संकट भी तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे सकते थे। इन संकटों को भी भारत ने राष्ट्र संघ के माध्यम से सुलझाया। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने दायित्व को भली-भाँति समझते हुए ईरान-इराक युद्ध की समाप्ति, दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की नीति को समाप्त करने और नामीबिया की स्वतन्त्रता और उपनिवेशवाद के अन्त से सम्बन्धित अनेक कार्यों के लिए निरन्तर प्रयत्न किये। इस प्रकार भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को शान्ति और सुरक्षा के कार्यों में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया गया।
लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। [2015, 16]
या
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। [2010, 15]
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का संगठन
महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्त्वपूर्ण अंग है। इसे ‘विश्व संसद’ के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें अपने पाँच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किन्तु किसी भी निर्णायक मतदान के अवसर पर उन पाँचों का केवल एक ही मत माना जाता है। इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितम्बर में होता है। यद्यपि इसके बहुमत अथवा सुरक्षा परिषद् के आग्रह पर संघ का महासचिव विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। इसके अतिरिक्त एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा सात उपाध्यक्ष संघ के पदाधिकारी होते हैं। महासभा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर विचार कर सकती है। साधारण विषयों में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किन्तु विशेष विषयों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत की विजयलक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –
- यह अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
- सुरक्षा परिषद् अपने 10 अस्थायी तथा सामाजिक, आर्थिक परिषद् के 54 सदस्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है।
- विश्व शान्ति के लिए आवश्यक विषयों पर सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकर्षित कराती है।
प्रश्न 2.
निषेधाधिकार (वीटो पावर) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पाँचों स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद् में किए गए निर्णय से सहमत नहीं, तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है।
प्रश्न 3.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताइए।
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को आविर्भाव सन् 1945 ई० में हुआ जिसे विश्व न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय नीदरलैण्ड की राजधानी हेग में स्थित है।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद् के बहुमत से की जाती है।
![]()
प्रश्न 4.
सुरक्षा परिषद् के चार महत्त्वपूर्ण कार्य बताइए। [2007, 10]
उत्तर :
सुरक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जाँच करना और उसके निराकरण के शान्तिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना।
- युद्ध को तत्काल बन्द करने के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना।
- महासभा को नए सदस्यों के सम्बन्ध में सुझाव देना।
- अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों को महासभा के पटल पर रखना।
प्रश्न 5.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय में बताइए।
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि झेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र महासभा के लिए 5 प्रतिनिधि, 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि तथा अनिश्चित संख्या में अपने सलाहकार भेज सकता है। लेकिन प्रत्येक देश को चाहे वह छोटा हो या बड़ा, महासभा में मात्र एक मत देने का ही अधिकार प्राप्त है। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 51 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 193 हो गयी है।
प्रश्न 6.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर :
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह स्वास्थ्य कार्यों से सम्बन्धित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है।
स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था अनेक कार्य करती है; जैसे-राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकटकाल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएँ बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना आदि।
प्रश्न 7.
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (IMF) कब स्थापित किया गया था तथा इसका क्या उद्देश्य था?
उतर :
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना दिसम्बर, 1945 ई० में की गयी थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी० सी० में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, व्यापार के सन्तुलित विकास को प्रोत्साहित करना, सदस्यों के मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ाना तथा उस सम्बन्ध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, विदेशी विनिमय-प्रतिबन्धों को हटाना, सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना तथा सदस्यों के मध्य भुगतान से अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन में असमानताओं को कम करना आदि हैं।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। [2012]
उत्तर :
- महासभा
- सुरक्षा परिषद्
- सामाजिक और आर्थिक परिषद्
- सचिवालय
- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा
- संरक्षण परिषद्।
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। [2007, 10]
उत्तर :
- विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना करना।
- नागरिकों की समानता एवं आत्म-निर्णय के अधिकार के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।
प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र संघ की उस संस्था का नाम लिखिए जो जन-स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है।
उत्तर :
अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.)।
प्रश्न 4.
सुरक्षा परिषद् में कितने सदस्य होते हैं ? [2009, 11, 12]
उत्तर :
पन्द्रह सदस्य।
प्रश्न 5 :
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या बताइए।
या
सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। [2008, 09, 10, 12]
उत्तर :
सुरक्षा परिषद् में पाँच स्थायी सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तथा साम्यवादी चीन हैं।
प्रश्न 6.
सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर :
सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है।
प्रश्न 7.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
उत्तर :
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है।
प्रश्न 8.
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं ? [2011, 14, 16]
उत्तर :
बान-की-मून।
![]()
प्रश्न 9
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखिए। [2016]
उत्तर :
अमेरिका, रूस।
प्रश्न 10.
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? [2007, 15, 16]
उत्तर :
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में।
प्रश्न 11.
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के दो गैर-यूरोपियन स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। [2008, 14]
उत्तर :
चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद् के दो गैर-यूरोपियन स्थायी सदस्य हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई – [2008, 13]
(क) 20 जनवरी, 1946 को
(ख) 24 अक्टूबर, 1945 को
(ग) 13 दिसम्बर, 1945 को
(घ) 1 जनवरी, 1946 को
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? [2007, 10]
(क) पेरिस में
(ख) लन्दन में
(ग) न्यूयॉर्क में
(घ) मास्को में
प्रश्न 3.
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(क) न्यूयॉर्क में
(ख) वाशिंगटन डी० सी० में
(ग) पेरिस में
(घ) हेग में
प्रश्न 4.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है?
(क) हेग में
(ख) पेरिस में
(ग) न्यूयॉर्क में
(घ) लन्दन में
प्रश्न 5.
निम्नलिखित में से कौन-सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है? [2012]
(क) इंग्लैण्ड
(ख) अमेरिका
(ग) रूस
(घ) भारत
प्रश्न 6.
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है – [2007]
(क) पाँच
(ख) दस
(ग) पन्द्रह
(घ) बारह
प्रश्न 7.
निम्नलिखित में से कौन-सा सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है?
(क) ब्रिटेन
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ग) फ्रांस
(घ) जर्मनी
प्रश्न 8.
संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
(क) 181
(ख) 190
(ग) 193
(घ) 201
प्रश्न 9.
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था नहीं है? [2007]
(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन
(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
प्रश्न 10.
किस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है ? [2008, 10, 14]
(क) 1 मई
(ख) 1 दिसम्बर
(ग) 24 अक्टूबर
(घ) 6 अगस्त
प्रश्न 11.
सुरक्षा परिषद् में कुल कितने सदस्य हैं? [2007, 09, 11, 12, 13]
(क) 5
(ख) 10
(ग) 15
(घ) 20
प्रश्न 12.
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है [2012]
(क) सुरक्षा परिषद्
(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन
(ग) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
प्रश्न 13.
निम्नलिखित में से कौन-सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं है? [2012]
(क) इंग्लैण्ड
(ख) अमेरिका
(ग) रूस
(घ) भारत
प्रश्न 14.
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? [2015]
(क) सन् 1942
(ख) सन् 1945
(ग) सन् 1946
(घ) सन् 1947
उत्तर :
- (ख) 24 अक्टूबर, 1945 को
- (ग) न्यूयॉर्क में
- (ख) वाशिंगटन डी० सी० में
- (क) हेग में
- (घ) भारत
- (ख) दस
- (घ) जर्मनी
- (ग) 193
- (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन
- (ग) 24 अक्टूबर
- (ग) 15
- (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन
- (घ) भारत
- (ख) सन् 1945।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Civics संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Civics संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.