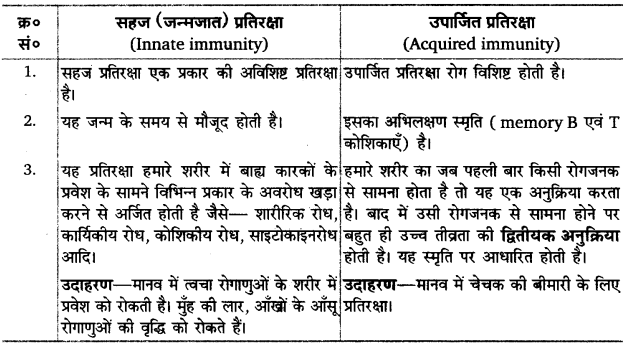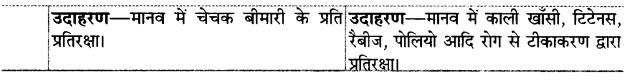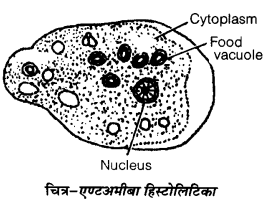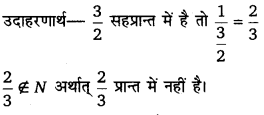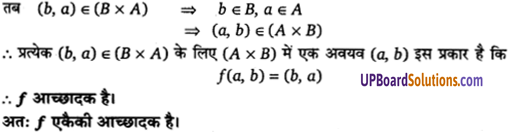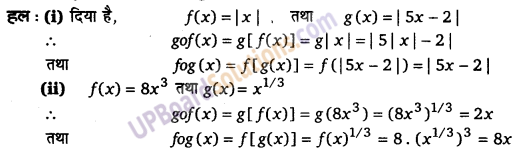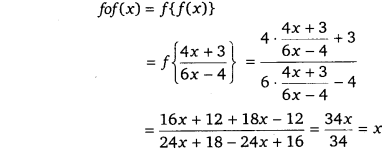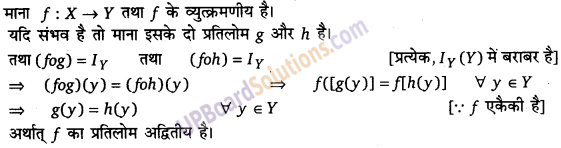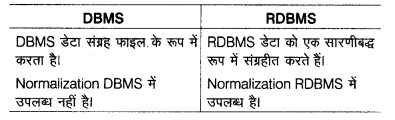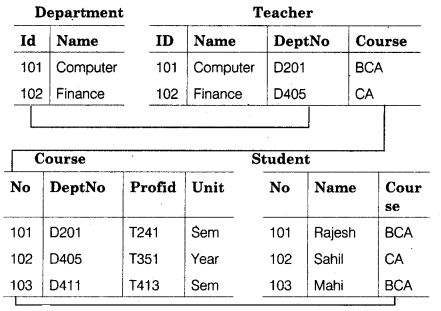UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 6 Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण) are part of UP Board Solutions for Class 12 Physics. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 6 Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Physics |
| Chapter | Chapter 6 |
| Chapter Name | Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण) |
| Number of Questions Solved | 54 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 6 Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण)
अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
चित्र 6.1 (a) से (f) में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति (predict) कीजिए।

उत्तर-
(a) चुम्बक के S ध्रुव को कुण्डली की ओर ले जाया जा रहा है, अत: लेन्ज के नियम के अनुसार कुण्डली का इस ओर का सिरा भी S ध्रुव होना चाहिए ताकि यह चुम्बक की गति का विरोध करे (परस्पर प्रतिकर्षण द्वारा) इसलिए कुण्डली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात् qrpq दिशा में बहेगी।
(b) चुम्बक की गति के विरोध के लिए लेन्ज नियम के अनुसार बायीं ओर की कुण्डली का चुम्बक के ध्रुव S की ओर वाला सिरा S बनना चाहिए तथा दायीं ओर की कुण्डली का (UPBoardSolutions.com) चुम्बक में N ध्रुव की ओर वाला सिरा भी S ध्रुव ही बनना चाहिए ताकि ध्रुव S पर प्रतिकर्षण तथा N पर आकर्षण बल लगे। इसलिए बायीं ओर की कुण्डली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में (अर्थात् prqp दिशा में), तथा दायीं ओर की कुण्डली में धारा yzxy दिशा में प्रेरित होनी चाहिए।
(c) दाब कुंजी तुरन्त बन्द करने पर बायीं ओर कुण्डली में धारा शून्य से बढ़ेगी, अत: दायीं ओर की कुण्डली में प्रेरित धारा बायीं ओर कुण्डली में धारा की विपरीत दिशा में (अर्थात् वामावर्त दिशा में) yzx में होनी चाहिए।
(d) चित्र से स्पष्ट है कि धारा नियन्त्रक द्वारा प्रतिरोध घटाया जा रहा है अर्थात् दायीं ओर कुण्डली में धारा बढ़ेगी जिसकी दिशा वामावर्त है। अतः लेन्ज के नियम के अनुसार (UPBoardSolutions.com) बायीं ओर कुण्डली में प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होनी चाहिए अर्थात् zyx दिशा में।
(e) दाब कुंजी को खोलने के तुरन्त बाद प्राथमिक कुण्डली में धारा घटेगी। अतः द्वितीयक कुण्डली में धारा की दिशा प्राथमिक के मुख्य धारा की दिशा में होनी चाहिए अर्थात् xry दिशा में।
(f) कोई प्रेरित धारा नहीं चूँकि बल रेखाएँ लूप के तल में स्थित होंगी तथा फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। चूँकि बल-रेखाएँ लूप को काटेंगी भी नहीं।
![]()
प्रश्न 2.
चित्र 6.2 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए।
(a) जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो;
(b) जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे तार में विरूपित किया जा रहा हो।

उत्तर-
(a) क्रॉस (x) द्वारा एक ऐसे चुम्बकीय-क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है जिसकी दिशा कागज के तल के लम्बवत् भीतर की ओर है अनियमित आकार के लूप को वृत्तीय (UPBoardSolutions.com) रूप में खींचने पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। अतः लूप में प्रेरित धारा इस प्रकार की होगी कि वह निम्नगामी फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगी। प्रेरित धारी कागज के तल के लम्बवत् ऊपर की ओर चुम्बकीय-क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अत: धारा की दिशा a d c b a मार्ग का अनुसरण करेगी।
(b) चुम्बकीय-क्षेत्र कागज के तल के लम्बवत् (UPBoardSolutions.com) बाहर की ओर है। लूप के आकार को बदलने पर उससे गुजरने वाला ऊर्ध्वमुखी फ्लक्स घटेगा। अत: लूप में प्रेरित धारा ऊर्ध्वमुखी चुम्बकीय-क्षेत्र उत्पन्न करेगी। इसके लिए धारा a’d’c’b’a’ मार्ग का अनुसरण करेगी।
प्रश्न 3.
एक लम्बी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लम्बाई में 15 फेरे हैं। उसके अन्दर 2.0 cm का एक छोटा-सा लूप परिनालिका की अक्ष के लम्बवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 0.15 में 2.0 A से 40 A कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा?


प्रश्न 4.
एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएँ 8 cm एवं 2 cm हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलम्बवत 0.3 T के एकसमान चुम्बकीय-क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 cm s-1 है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, जब लूप की गति अभिलम्बवत हो
(a) लूप की लम्बी भुजा के
(b) लूप की छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी?
हल-
(a) चुम्बकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लम्बवत् स्थित क्षेत्रफल A से गुजरने वाला चुम्बकीय फ्लक्स Φ = BA
माना लूप की लम्बाई l व चौड़ाई b है तथा (UPBoardSolutions.com) इसके वेग का परिमाण है। जैसे ही लूप लम्बी भुजा के लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर निकालता है क्षेत्र से बद्ध क्षेत्रफल बदलता है, जिससे में परिवर्तन होता है। फैराडे के नियम से, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण


![]()
प्रश्न 5.
1.0 m लम्बी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलम्बवत अक्ष के परितः 400 rad-s-1 की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से सम्पर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 T का एकसमान चुम्बकीय-क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए।

प्रश्न 6.
एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 cm तथा फेरों की संख्या 20 है अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 rad-s- की कोणीय आवृत्ति से 3.0 x 10-2 T के एकसमान चुम्बकीय-क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली 10 Ω प्रतिरोध का एक बन्द लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है?


कुण्डली में प्रेरित धारा एक बल-आघूर्ण उत्पन्न करती है, जो कुण्डली के घूमने का विरोध करता है। इसलिए कुण्डली को एकसमान कोणीय वेग से (UPBoardSolutions.com) घुमाए रखने के लिए एक बाह्य कारक (रोटर) बल-आघूर्ण प्रदान करता है। इसीलिए व्यय ऊष्मा का स्रोत रोटर (rotor) ही है।
प्रश्न 7.
पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 m लम्बा क्षैतिज सीधा तार 0.30 x 10-4 Wbm-2 तीव्रता वाले पृथ्वी के चुम्बकीय-क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लम्बवत 5.0 m s-1 की चाल से गिर रहा है।
(a) तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा?
(b) विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है?
(c) तार का कौन-सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है?
हल-
(a) तार की लम्बाई l = 10 मीटर, B = H = 0.30 x 10-4 वेबर/मी2, तार का वेग v = 50 मी/सेकण्ड
अतः तार के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर e = Bvl sin 90° = Bvl = 0.30 x 10-4 x 5.0 x 10 = 0.0015 वोल्ट = 1.5 मिलीवोल्ट
(b) फ्लेमिंग के दायें हाथ के नियम के अनुसार, तार में प्रेरित धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। अतः प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी।
(c) चूँकि तार में प्रेरित धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, अत: तार में इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव (UPBoardSolutions.com) से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, अत: तार का पूर्वी सिरा उच्च विभव पर होगा। [विशेष-यदि तार उत्तर-दक्षिण दिशा में रहते हुए गिरता, तब इसकी लम्बाई पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान्तर होती। अतः कोई वैद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता।
![]()
प्रश्न 8.
किसी परिपथ में 0.1 s में धारा 5.0 A से 0.0 A तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 V है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए।


प्रश्न 9.
पास-पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 H है। यदि एक कुंडली । में 0.5 s में धारा 0 से 20 A परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा?
हल-
यहाँ M = 1.5 हेनरी, ∆t = 0.5 सेकण्ड,
∆I = I2 – I1 = (20 – 0) = 20 A
Φ1 = MI
∆Φ2 = M∆I1
अतः द्वितीयक कुण्डली की फ्लक्स बद्धता में परिवर्तन
∆Φ2 = 1.5 हेनरी x 20 ऐम्पियर = 30 वेबर
यहाँ धारा बढ़ रही है, अत: फ्लक्स बद्धता में परिवर्तन धारा वृद्धि का विरोध करेगा।
प्रश्न 10.
एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 km/h वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 m लम्बे हैं। इनके सिरों पर कितना विभवान्तर उत्पन्न होगा? पृथ्वी के चुम्बकीय-क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 x 10-4 Tतथा नति कोण (dip angle) 30° है।

अतिरिक्त अभ्यास
प्रश्न 11.
मान लीजिए कि प्रश्न 4 में उल्लिखित लूप स्थिर है किन्तु चुम्बकीय-क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुम्बक में धारा का मान कम किया जाता है जिससे चुम्बकीय-क्षेत्र का मान अपने प्रारम्भिक मान 0.3 T से 0.02 Ts-1 की दर से घटता है। अब यदि लूप का कटा भाग जोड़ दें जिससे प्राप्त बन्द लूप का प्रतिरोध 1.6 Ω हो तो इस लूप में ऊष्मन के रूप में शक्ति ह्रास क्या है? इस शक्ति का स्रोत क्या है?

प्रश्न 12.
12 cm भुजा वाला वर्गाकार लूप जिसकी भुजाएँ X एवं Y अक्षों के समान्तर हैं, x-दिशा में 8 cm s-1 की गति से चलाया जाता है। लूप तथा उसकी गति का परिवेश धनात्मक दिशा के चुम्बकीय-क्षेत्र का है। चुम्बकीय-क्षेत्र न तो एकसमान है और न ही समय के साथ नियत है। इस क्षेत्र की (UPBoardSolutions.com) ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10-3 Tcm-1 है। (अर्थात् ऋणात्मक x-अक्ष की दिशा में इकाई सेंटीमीटर दूरी पर क्षेत्र के मान में 10-3 Tcm-1 की वृद्धि होती है) तथा क्षेत्र के मान में 10-3 Ts-1 की दर से कमी भी हो रही है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4.50 mΩ हो तो प्रेरित धारा का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए।


प्रश्न 13.
एक शक्तिशाली लाउडस्पीकर के चुम्बक के ध्रुवों के बीच चुम्बकीय-क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मापन किया जाना है। इस हेतु एक छोटी चपटी 2 cm क्षेत्रफल की अन्वेषी कुंडली (search coil) का प्रयोग किया गया है। इस कुंडली में पास-पास लिपटे 25 फेरे हैं तथा इसे चुम्बकीय-क्षेत्र के लम्बवत व्यवस्थित किया गया है और तब इसे द्रुत गति से क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। तुल्यतः एक अन्य विधि में अन्वेषी कुंडली को 90° से तेजी से घुमा देते हैं जिससे कुंडली का तल चुम्बकीय-क्षेत्र के समान्तर हो जाए। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 mC आवेश का प्रवाह होता है (जिसे परिपथ में प्रक्षेप धारामापी (ballistic galvanometer) लगाकर ज्ञात किया जा सकता है)। कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध 0.50 Ω है। चुम्बक की क्षेत्र की तीव्रता का आकंलन कीजिए।


![]()
प्रश्न 14.
चित्र 6.6 में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है जो पटरियों AB पर रखी है तथा एक स्थायी चुम्बक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। पटरियाँ, छड़ एवं चुम्बकीय-क्षेत्र परस्पर अभिलम्बवत दिशाओं में हैं। एक गैल्वेनोमीटर (धारामापी) G को पटरियों से एक स्विच K की सहायता से संयोजित किया गया है। छड़ की लम्बाई = 15 cm, B = 0.50 T तथा पटरियों, छड़ तथा धारामापी से बने बन्द लूप का प्रतिरोध = 9.0 m2 है। क्षेत्र को एकसमान मान लें।
(a) माना कुंजी Kखुली (open) है तथा छड़ 12 cm s-1 की चाल से दर्शायी गई दिशा में गतिमान है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एवं ध्रुवणता (polarity) बताइए।

(b) क्या कुंजी Kखुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी K बंद (close) कर दी जाए?
(c) जब कुंजी K खुली हो तथा छड़ एकसमान वेग से गति में हो तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता यद्यपि उन पर छड़ की गति के कारण चुम्बकीय बल कार्य करता है। कारण स्पष्ट कीजिए।
(d) कुंजी बन्द होने की स्थिति में छड़ पर (UPBoardSolutions.com) लगने वाले अवमन्दन बल का मान क्या होगा?
(e) कुंजी बन्द होने की स्थिति में छड़ को उसी चाल (= 12 cms-1) से चलाने हेतु कितनी शक्ति (बाह्य कारक के लिए) की आवश्यकता होगी?
(f) बन्द परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा? इस शक्ति का स्रोत क्या है?
(g) गतिमान छड़ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा यदि चुम्बकीय-क्षेत्र की दिशा पटरियों के लम्बवत होने की बजाय उनके समान्तर हो?
हल-
दिया है, B = 0.50 T, l = 0.15 m, v = 0.12 m s-1, R = 9.0 x 10-3
(a) छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल
e = Bvl = 0.50 x 0.12 x 0.15 = 9 x 10-3 V = 9.0 mV
छड़ का सिरा P धनात्मक तथा २ ऋणात्मक होगा।
(b) हाँ, छड़ के Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन एकत्र हो जाएँगे जबकि P सिरे पर धनावेश की अधिकता हो जाएगी। यदि कुंजी K को बन्द कर दिया जाए तो सिरे पर एकत्र होने वाले इलेक्ट्रॉन बन्द परिपथ से होते हुए (G से होकर) सिरे P की ओर गति करने लगेंगे। इस प्रकार परिपथ में स्थायी धारा स्थापित हो जाएगी।
(c) जब कुंजी K खुली है तो P सिरा धनात्मक व Q सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इससे छड़ के भीतर सिरे P से सिरे २ की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थित हो जाता है। (UPBoardSolutions.com) इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर Q से P की ओर विद्युत बल लगता है जो विपरीत दिष्ट चुम्बकीय बल को सन्तुलित कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों पर कोई नैट बल कार्य नहीं करता है।
(d) कुंजी K बन्द होने की स्थिति छड़ PQ से प्रवाहित धारा

(e) कुंजी K के बन्द होने पर छड़ को खींचते रहने के लिए व्यय की जाने वाली शक्ति
P = Fv = 0.075 x 0.12 = 9 x 10-3 W
(f) परिपथ में व्यय ऊष्मीय शक्ति
P = R= (1.0) x 9.0 x 10-3 = 9 x 10-3 W
इस शक्ति का स्रोत छड़ को एकसमान वेग से खींचते रहने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा व्यय की गई शक्ति है।
(g) शून्य; इस स्थिति में छड़ चुम्बकीय बल रेखाओं को नहीं काटेगी।
अतः कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा।
प्रश्न 15.
वायु के क्रोड वाली एक परिनालिका में, जिसकी लम्बाई 30 cm तथा अनुप्रस्थ काट का कषेत्रफल 25 cm तथा कुल फेरे 500 हैं, 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को 10-38 के अल्पकाल में अचानक बन्द कर दिया जाता है। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? परिनालिका के सिरों पर चुम्बकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं ?

![]()
प्रश्न 16.
(a) चित्र 6.7 में दर्शाए अनुसार एक लम्बे, सीधे तार तथा एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा की लम्बाई a है, के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
(b) अब मान लीजिए कि सीधे तार में 50 A की धारा प्रवाहित हो रही है तथा लूप एक स्थिर वेग v = 10 m/s से दाईं ओर को गति कर रहा है। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिकलन चित्र 6.7 उंस क्षण पर कीजिए जब x = 0.2 m हो। लूप के लिए a = 0.1 m लीजिए तथा यह मान लीजिए कि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है।



प्रश्न 17.
किसी M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या वाले एक पहिए के किनारे (rim) पर एक रैखिक आवेश स्थापित किया गया है जिसकी प्रति इकाई लम्बाई पर आवेश का मान 2 है। पहिए के स्पोक (spoke) हल्के एवं कुचालक हैं तथा वह अपनी अक्ष के परितः घर्षण रहित घूर्णन हेतु स्वतन्त्र हैं जैसा कि चित्र 6.9 में दर्शाया गया है। पहिए के वृत्तीय भाग पर रिम, के अन्दर एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र विस्तरित है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है-


चुम्बकीय-क्षेत्र को अचानक ‘ऑफ (Switched off) करने के पश्चात्, पहिए का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए।
हल-
माना चुम्बकीय-क्षेत्र को स्विच ऑफ करने पर E विद्युत-क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा पहिया ω कोणीय वेग से घूमना प्रारम्भ करता है।
यदि पहिए पर कुल आवेश q है तो एक पूर्ण चक्र के दौरान विद्युत-क्षेत्र द्वारा आवेश को घुमाने में कृत कार्य


परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है- (2012, 15)
(i) लेन्ज के नियम द्वारा
(ii) फ्लेमिंग के बायें हाथ के नियम द्वारा
(iii) बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा
(iv) ऐम्पियर के नियम द्वारा
उत्तर-
(i) लेन्ज के नियम द्वारा
![]()
प्रश्न 2.
लेन्ज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? (2017, 18)
(i) आवेश
(ii) संवेग
(iii) ऊर्जा
(iv) द्रव्यमान
उत्तर-
(iii) ऊर्जा
प्रश्न 3.
लेन्ज के वैद्युत चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? (2010, 12, 13)
(i) आवेश का संरक्षण
(ii) चुम्बकीय फ्लक्स का संरक्षण
(iii) ऊर्जा का संरक्षण
(iv) संवेग का संरक्षण
उत्तर-
(iii) ऊर्जा का संरक्षण
प्रश्न 4.
हेनरी/मीटर मात्रक है-
(i) वैद्युतशीलता का
(ii) चुम्बकशीलता का
(iii) परावैद्युतक का
(iv) स्वप्रेरकत्व का
उत्तर-
(ii) चुम्बकशीलता का
प्रश्न 5.
[latex]\frac { L }{ R }[/latex] की विमा होगी, जहाँ प्रेरकत्व है तथा प्रतिरोध है- (2013,17)
(i) [M0L0T-1]
(ii) [M0LT]
(iii) [M0L0T]
(iv) [MLT-2]
उत्तर-
(iii) [M0L0T]
प्रश्न 6.
10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुण्डली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गयी है। कुण्डली में संचित ऊर्जा है- (2014)
(i) 125 जूल
(ii) 62.5 जूल
(iii)250 जूल
(iv) 500 जूल
उत्तर-
(iv) 500 जूल
![]()
प्रश्न 7.
एक कुण्डली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 mH है। उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 103 ऐम्पियर/सेकण्ड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। (2014)
(i) 1 वोल्ट
(ii) 2 वोल्ट
(iii) 3 वोल्ट
(iv) 4 वोल्ट
उत्तर-
(ii) 2 वोल्ट
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेन्ज का नियम क्या है? (2014, 16, 17)
उत्तर-
किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है।
प्रश्न 2.
भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? (2010, 12, 17, 18)
या
भंवर धाराएँ क्या होती हैं? (2013, 18)
उत्तर-
आँवर धाराएँ (Eddy Currents)- सन् 1875 में फोको (Focault) ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती” (variable) चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अथवा किसी चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के (UPBoardSolutions.com) सम्पूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएँ धातु के टुकड़े की गति का (अथवा फ्लक्स परिवर्तन का) विरोध करती हैं। इन धाराओं को ‘भंवर धाराएँ’ कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें ‘फोको धाराएँ’ भी कहा जाता है। कभी-कभी ये धाराएँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल-तप्त हो जाता है।
![]()
प्रश्न 3.
भंवर धाराओं से क्या हानियाँ हैं? किसी ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में इनको उत्पन्न होने से किस प्रकार रोका जा सकता है? (2017)
उत्तर-
ट्रांसफॉर्मर, डायनमो तथा मोटर की आमेचर कुण्डलियों की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती हैं। जब इन यन्त्रों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्रोड में भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय (UPBoardSolutions.com) ऊर्जा में हास होने लगता है। इस हास ( भंवर धाराओं) को कम करने के लिए क्रोड को नर्म लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में न लेकर, नर्म लोहे की कई पतली-पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़कर आवश्यक मोटाई बना लेते हैं। इस प्रकार की क्रोड, पटलित क्रोड (laminated core) कहलाती है। ऐसा करने से क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा मँवर धाराएँ क्षीण हो जाती हैं, फलस्वरूप ऊर्जा ह्रास कम हो जाता है।
प्रश्न 4.
चित्र 6.10 में एक दण्ड-चुम्बक मुक्त रूप से एक कुण्डली के बीच से होकर गिरता है। कारण सहित बताइए कि घुम्बक की त्वरण (a), गुरुत्वीय त्वरण(g) से कम अथवा समान अथवा अधिक होगा। (2015)

उत्तर-
जब एक दण्ड चुम्बक मुक्त रूप से एक कुण्डली के बीच से होकर गिरता है तो कुण्डली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जो सदैव उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह उत्पन्न होती है। अत: चुम्बक का त्वरण (a), गुरुत्वीय त्वरण (g) से कम होगा।
प्रश्न 5.
0.2 वेबर /मी के चुम्बकीय क्षेत्र में 10.0 सेमी पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुण्डली 20.0 रेडियन/से के नियत कोणीय वेग से घूम रही है। उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए (2013)
हल-
आयताकार कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स
Φ = BA = (0.2) x (10 x 10-4) वेबर = 2 x 10-4 वेबर
आयताकार कुण्डली 20.0 रेडियन/से के नियत कोणीय वेग से घूम रही है अर्थात् प्रत्येक चक्कर में फ्लक्स परिवर्तन कें होगा। चूंकि कुण्डली 1 सेकण्ड में 20 चक्कर पूरे कर रही है, अत: फ्लक्स परिवर्तन की दर 20Φ होगी जो कि अभीष्ट प्रेरित विवा० बल होगा।
अतः e = 20Φ = 20 x 2 x 10-4 वोल्ट = 4.0 x 10-3 वोल्ट = 4 मिलीवोल्ट
प्रश्न 6.
एक कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 0.1 सेकण्ड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। (2015)

प्रश्न 7.
1000 फेरों वाली एक कुण्डली में 2.5 ऐम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 1.4 x 10-4 वेबर है। कुण्डली का प्रेरकत्व क्या है? (2013)

प्रश्न 8.
एक कुण्डली से बढ़ चुम्बकीय फ्लक्स 0.1 सेकण्ड में 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। (2015)

![]()
प्रश्न 9.
अन्योन्य प्रेरण गुणांक की विमा लिखिए। (2011)
उत्तर-
[ML2T-2A-2].
प्रश्न 10.
स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? (2016)
या
स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। (2017)
उत्तर-
स्वप्रेरण- किसी कुण्डली से सम्बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुण्डली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्त्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र = [ML2T-2A-2]
प्रश्न 11.
स्वप्रेरण-गुणांक का विमा सूत्र लिखिए।
उत्तर-
[ML2T-2A-2]
प्रश्न 12.
8.0 मिली-हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुण्डली में 2.0 ऐम्पियर धारा है। कुण्डली के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है? (2010)

![]()
प्रश्न 13.
एक कुण्डली का स्वप्रेरकत्व 3.0 x 10-3 हेनरी है। यदि 0.1 सेकण्ड में कुण्डली की धारा का मान 5 ऐम्पियर से घट कर शून्य हो जाये तो कुण्डली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। (2011, 12)

प्रश्न 14.
एक कुण्डली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिलीसेकण्ड में 5 ऐम्पियर से 15 ऐम्पियर हो जाती है। कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। (2016, 18)

प्रश्न 15.
यदि प्राथमिक कुण्डली में बहने वाली 3.0 ऐम्पियर की धारा को 0.001 सेकण्ड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल 15000 वोल्ट होता है। इन कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। (2017)

लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
फ्लेमिंग का दायें हाथ का नियम लिखिए। (2011)
उत्तर-
फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम (Fleming’s Right Hand Rule)- जब कोई ऋजुरेखीय चालक तार किसी चुम्बकीय क्षेत्र में उसके लम्बवत् गति करता है तो इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दायें हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार, (UPBoardSolutions.com) यदि हम दायें हाथ का अँगूठा तथा इसके पास वाली दोनों अँगुलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएँ कि वे परस्पर लम्बवत् हों (चित्र 6.11), तब यदि पहली अँगुली चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अँगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करें तो बीच वाली अँगुली चालक में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी।”

प्रश्न 2.
फैराडे के वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण सम्बन्धी नियम बताइए। (2009, 11, 15, 17, 18)
उत्तर-
फैराडे के वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के नियम-फैराडे ने वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम दिये हैं
(i) प्रथम नियम- “जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।” यदि परिपथ ‘बन्द’ है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब
तक कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है।
(ii) द्वितीय नियम- “प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है।” यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स का मान के Φ1 है और Δt समयान्तर के बाद यह फ्लक्स हो जाता है, तो

ऋणात्मक चिह्न यह प्रदर्शित करता है कि वि० वा० बल सदैव चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह लेन्ज का नियम कहलाता है। यदि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर वेबर प्रति सेकण्ड में लें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होता है। यदि कुण्डली में N फेरे हों तो पूरी कुण्डली में प्रेरित वि० वा० बल

जहाँ, NΦ कुण्डली में चुम्बकीय फ्लक्स-ग्रन्थिताओं (flux linkages) की संख्या है।
प्रश्न 3.
भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। (2017, 18)
उत्तर-
आँवर धाराओं के अनुप्रयोग निम्नवत् हैं-
(i) दोलन-रुद्ध धारामापी- चल-कुण्डली धारामापियों को दोलन-रुद्ध (dead beat) बनाने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिये धारामापी की कुण्डली ताँबे के विद्युतरोधी तार को ऐलुमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनायी जाती है। जब कुण्डली विक्षेपित होती है, (UPBoardSolutions.com) तो उससे बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे फ्रेम में भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कुण्डली की गति का विरोध करती हैं। अत: कुण्डली शीघ्र ही शून्य पर लौट आती है।
(ii) प्रेरण भट्टी- प्रेरण भट्टी में पिघलाये जाने वाली धातु को एक तेजी से परिवर्तित होने वाले चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसे उच्च-आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा से प्राप्त किया जाता है इससे धातु में प्रबल भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी ऊष्मा से धातु लाल-तप्त होकर पिघल जाती है। यह प्रक्रिया खनिज पदार्थ से धातु निकालने में भी प्रयुक्त की जाती है।
(iii) प्रेरण मोटर- जब एक धात्विक बेलन किसी घूमते हुए चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो बेलन में भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएँ, लेन्ज के नियमानुसार, (UPBoardSolutions.com) बेलन तथा चुम्बकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति को घटाने का प्रयत्न करती हैं। अतः बेलन चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। प्रेरण मोटर का यही सिद्धान्त है।
(iv) वैद्युत ब्रेक- विद्युत रेलगाड़ियों में पहिये की धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है जो पहिये के साथ घूमता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं, तो ड्रम पर एक प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। जिससे ड्रम में भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं और ड्रम पहिये को रोक देता है।
![]()
प्रश्न 4.
एक कुण्डली का क्षेत्रफल 100 सेमी है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर/मी2 का चुम्बकीय क्षेत्र कुण्डली के तल के लम्बवत है। यदि चुम्बकीय क्षेत्र 0.1 सेकण्ड में घटकर शुन्य हो जाए तो कुण्डली में प्रेरित वि० वा० बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुण्डली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। (2013, 14)

प्रश्न 5.
एक L लम्बाई की धातु की छड़ कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। चुम्बकीय क्षेत्र B छड़ की घूर्णन अक्ष के समान्तर आरोपित है। छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि छड़ का प्रतिरोध हो तब उसमें प्रेरित धारा क्या होगी? (2014)

प्रश्न 6.
जब एक प्राथमिक कुण्डली में धारा शून्य से 2.0 ऐम्पियर, 300 मिली सेकण्ड में परिवर्तित की जाती है तो द्वितीयक कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है। दोनों कुण्डलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। (2015)

प्रश्न 7.
स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। (2009, 11, 13, 16, 17, 18)
या
स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। (2013, 14, 17)
उत्तर-
NΦ = Li तथा यदि i = 1 तो L = NΦ, अत: किसी कुण्डली का स्वप्रेरण गुणांक कुण्डली में चुम्बकीय फ्लक्स ग्रन्थिताओं के बराबर होता है, जबकि कुण्डली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण

अत: “किसी कुण्डली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक (UPBoardSolutions.com) रूप से उस प्रेरित वि० वा० बल के बराबर होता है जो कुण्डली में धारा-परिवर्तन की दर एकांक अर्थात् एक ऐम्पियर प्रति सेकण्ड होने पर उत्पन्न होता है।” इसका मात्रक हेनरी होता है।
प्रश्न 8.
एक समतल वृत्ताकार कुण्डली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। (2012)
उत्तर-
माना r मीटर त्रिज्या तथा N फेरों की एक समतल वृत्ताकार कुण्डली में ऐम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अतः कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र

मानी कुण्डली के सम्पूर्ण तल में चुम्बकीय क्षेत्र B एकसमान है (यद्यपि कुण्डली की परिधि के समीप चुम्बकीय क्षेत्र B अधिक होता है)। अतः कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय-फ्लक्स Φ = BA
जहाँ, A कुण्डली के तल का क्षेत्रफल है; अतः A = πr²
समीकरण (1) से B का मान रखने पर,

समीकरण (1) से स्पष्ट है कि किसी कुण्डली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाने के लिए कुण्डली में फेरों की संख्या अधिक लेनी चाहिए। यदि कुण्डली के अन्दर. लौहचुम्बकीय पदार्थ की छड़ रख दी जाए तो कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय-फ्लक्स बढ़ जाता है, जिससे कुण्डली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा।
प्रश्न 9.
धारावाही लम्बी परिनालिका के स्व-प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। (2017, 18)
उत्तर-
माना एक लम्बी वायु-क्रोड परिनालिकों की लम्बाई l तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। परिनालिका में फेरों की कुल संख्या N तथा उसमें प्रेरित धारा i है।


प्रश्न 10.
स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। (2018)
एक प्रेरक में प्रवाहित धारा i = 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ i ऐम्पियर तथा t सेकण्ड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए।
(i) स्वप्रेरण गुणांक तथा
(ii) t = 2 सेकण्ड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा
हल-
[स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न 7 का उत्तर देखें।]
दिया है,
e = 10 मिलीवोल्ट = 10 x 10-3 वोल्ट

प्रश्न 11.
एक प्रेरकत्व कुण्डली में वैद्युत धारा 0.3 सेकण्ड में शून्य से बढ़कर 8.0 A हो जाती है। जिसके कारण उसमें 30 V का प्रेरित वि० वा० बल उत्पन्न हो जाता है। कुण्डली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। (2014)

प्रश्न 12.
किसी कुण्डली में 0.1 सेकण्ड में धारा शून्य से बढ़कर 5.0 ऐम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुण्डली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। (2016)
हल-
दिया है, समयान्तराल ∆t = 0.1 सेकण्ड
प्रेरित विद्युत वाहक बल, e = 20 वोल्ट
धारा परिवर्तन, ∆i = (5 – 0) = 5 ऐम्पियर

प्रश्न 13.
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। किसी कुण्डली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुण्डली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 ऐम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जायेगा? (2015)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
संक्षेप में बताइए कि लेन्ज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धान्त को कैसे पोषित करता है। (2009)
या
लेन्ज का नियम लिखिए। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धान्त का उल्लंघन करता है? (2009, 11)
या
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सम्बन्धी लेन्ज के नियम का उल्लेख कीजिए। यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? (2015)
या
लेन्ज का नियम क्या है? (2018)
उत्तर-
लेन्ज का नियम- किसी परिपथ में प्रेरित वि० वा० बल, अथवा प्रेरित धारा, की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होती है। इसे ही ‘लेन्ज का नियम’ कहते हैं। लेन्ज के नियम की पुष्टि फैराडे के प्रयोगों से हो जाती है। इन प्रयोगों में (UPBoardSolutions.com) चुम्बक की गति के कारण ही कुण्डली में प्रेरित धारा बहती है। जब हम चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुण्डली के पास लाते हैं तो कुण्डली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होती है कि कुण्डली का चुम्बक के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है (चित्र 6.12 a)। अतः यह पास आते हुए चुम्बक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है अर्थात् उसकी गति का विरोध करता है। इसी प्रकार, जब चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को।
कुण्डली से दूर हटाते हैं तो कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुण्डली का सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है (चित्र 6.12 b)। अब यह चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित करता है अर्थात् उसकी गति को पुन: विरोध करता है। ठीक इसी प्रकार, जब चुम्बक के दक्षिणी ध्रुव को कुण्डली के पास ले जाते हैं अथवा दूर हटाते हैं तो कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है (UPBoardSolutions.com) कि वह चुम्बक की गति का विरोध करती है (चित्र 6.12 c तथा d)। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक दंशा में चुम्बक को गतिमान करने के लिए इस विरोधी बल के कारण कुछ यान्त्रिक कार्य करना पड़ता है। ऊर्जा-संरक्षण के नियमानुसार, ठीक यही कार्य हमें कुण्डली में वैद्युत-ऊर्जा (ऊष्मा) के रूप में प्राप्त होता है।
हम चुम्बक को जितना तेज चलायेंगे हमें उतनी ही तेजी से कार्य करना होगा अर्थात् प्रेरित धारा उतनी ही प्रबल होगी। यदि कुण्डली किसी स्थान पर कटी हो (परिपथ खुला हो) तब चुम्बक को चलाने पर धारा प्रेरित नहीं होगी (यद्यपि वि० वा० बल प्रेरित होगा) तथा कोई कार्य भी नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रयोगों में यह बात उल्लेखनीय है कि यदि कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा चुम्बक की गति का विरोध न करे तो हमें बिना कोई कार्य किये ही लगातार वैद्युत-ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी जो कि असम्भव है। अतः लेन्ज का नियम ऊर्जा-संरक्षण के लिए एक आवश्यकता है।
![]()
प्रश्न 2.
वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है ? वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। (2011, 17)
या
अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुण्डलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। (2012)
या
अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। (2015, 17)
उत्तर-
वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)- जब किसी कुण्डली तथा चुम्बक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुण्डली में एक वि० वा० बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुण्डली एक बन्द परिपथ में है तो इस प्रेरित वि० वा० बल के कारण (UPBoardSolutions.com) कुण्डली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं।

अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction)- यदि दो कुण्डलियों को पास-पास रखकर, एक में धारा प्रवाहित करें, अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बन्द करे, अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुण्डली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण की (UPBoardSolutions.com) यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। वह कुण्डली जिसमें धारा परिवर्तित होती है, प्राथमिक कुण्डली तथा जिसमें प्रेरित वि० वा० बल उत्पन्न होता है, द्वितीयक कुण्डली कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण के उदाहरण ट्रांसफॉर्मर तथा प्रेरण कुण्डली हैं।
अन्योन्य प्रेरण-गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व– (i) यदि प्राथमिक कुण्डली में ip ऐम्पियर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीयक कुण्डली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स Φs, हो और द्वितीयक कुण्डली में कुल Ns फेरे हों, तो द्वितीयक कुण्डली से बद्ध कुल चुम्बकीय फ्लक्स NsΦs होगा, जो प्राथमिक कुण्डली में प्रवाहित धारा ip के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात्

अत: ‘दो कुण्डलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण-गुणांक किसी एक कुण्डली के उस प्रेरित वि० वी० बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुण्डली में धारा-परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है।” अन्योन्य प्रेरण-गुणांक का मात्रक हेनरी है तथा विमा [ML2T-2A-2] है।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 6 Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Physics Chapter 6 Electromagnetic Induction (वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.