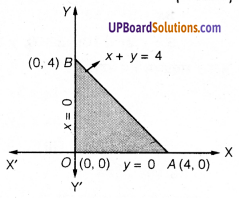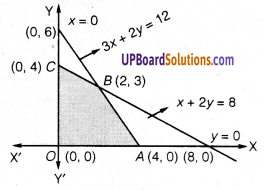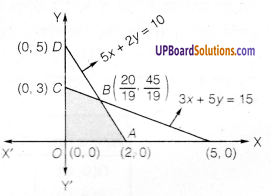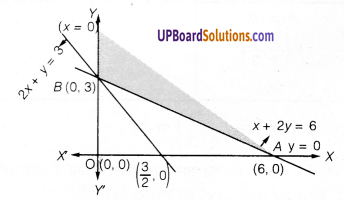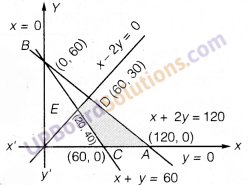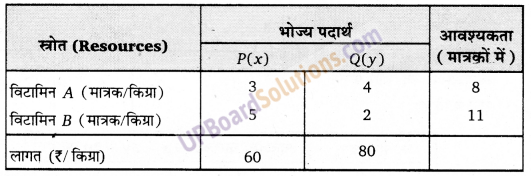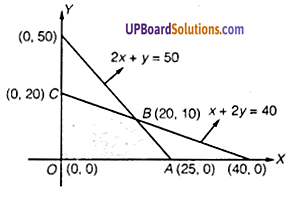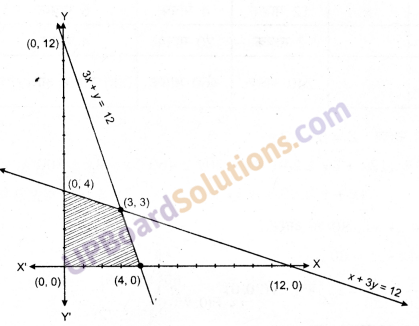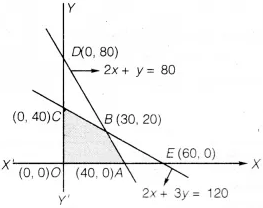UP Board Solutions for Class 12 English Prose Chapter 6 Women’s Education are part of UP Board Solutions for Class 12 English. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 English Prose Chapter 6 Women’s Education.
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | English Prose |
| Chapter | Chapter 6 |
| Chapter Name | Womens Education |
| Number of Questions Solved | 18 |
| Category | NCERT Solutions |
UP Board Class 12th English Prose Chapter 6 Women’s Education Questions and Answers
English Class 12 UP Board Chapter 6 Question Answer
कक्षा 12 अंग्रेजी पाठ 6 के प्रश्न उत्तर
LESSON at a Glance
We are living in an age where there are great opportunities for women in social work, public life and administration. Society needs women of disciplined minds and restrained manners. Hence, women’s education is of paramount importance in present time.
Dr. Radhakrishnan is not satisfied with the type of education that Indian women are getting. Girls education is not widespread so the institutions imparting education to girls should be encouraged. The education, so imparted, must not only be broad but should also be deep and purposeful.
According to the author, compassion, daya, is the quality which is more characteristic of women than of men. It is therefore, essential for every human being, men and women alike, to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. Without these qualities we are only human animals, nara pasu, not more than that.
Dr, Radhakrishnan says that the study of our great classics, such as the Ramayana, Upnishad, etc., and communion with great minds, are the two things that mould men’s mind and heart. They instil into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. The learned author realises the value of women’s education and says.
“Give us good women, we will have a great civilization.
Give us good mothers, we will have a great nation.”
Such is the importance of women’s education.
पाठ का हिन्दी अनुवाद
(1) You are living ………………. your work.
आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य में, जनजीवन में तथा प्रशासन में अनेक महान् अवसर प्राप्त हैं। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली तथा संयमित आचरण वाली स्त्रियाँ चाहिए। आप चाहे कोई भी कार्य चुनें आपको उसे ईमानदारी तथा अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। तभी आपको कार्य में सफलता और आनन्द प्राप्त होंगे।
(2) Actually in our ………………. present generation.
हिन्दी अनुवाद–वास्तव में, हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा काफी विस्तृत नहीं है। इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है वह मान्यता, उत्साह प्रदान करने के योग्य है। लेकिन मैं इस बात के लिए चिन्तित हूँ कि जो शिक्षा प्रदान की जाए वह केवल विस्तृत ही ने हो, अपितु वह जीवन के रहस्यों को जानने के योग्य भी हो। इसे गहराई में अर्थात् जीवन के रहस्यों को जानने में हम पीछे हैं। हम विद्वान् और कुशल बन सकते हैं। किन्तु यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तब हमारा जीवन अन्धकारमय होगा, हम भारी भूलें करेंगे और फिर हमें दुःख प्राप्त होगा। गीता में कहा है। ‘व्यावसायात्मिका बुद्धिरेकेह’ अर्थात् नि:स्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है और एक ओर ही लगी रहती है। एक सच्चे सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य को मानसिक एकरूपता तथा जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेम होता
है। एक असंस्कृत मनुष्य के लिए सम्पूर्ण जीवन भिन्न-भिन्न दिशाओं में बिखरा रहता है—“बहुशाखा ह्यनन्ताश्च’। अत: यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं, वह आपको केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे, अपितु आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी दे। वह निश्चित उद्देश्य क्या हो यह आपको सोचना है। यह कहा जाता है कि विद्या विवेक प्रदान करती है। विमर्शरूपिणी विद्या आपको यह ज्ञान प्रदान करती है कि जिससे आप यह तय करेंगे कि क्या उचित है। वह आपको अनुचित बातों से बचने में सहायता करेगी। इसलिए आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षित है। एक वह उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है, वह हमारे देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में ठीक नहीं भी हो सकता। इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपनाएँ, वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
(3) Every time we ………………. more than that.
जब भी हम कोई कार्य आरम्भ करते हैं तब हम अपने मन्त्रों का उच्चारण करते हैं और उस कार्य को समाप्त करते समय शान्ति-शान्ति कहते हैं। अध्यापक तथा शिष्यों से यह आशा की जाती है कि वे एक-दूसरे से घृणा करने से बचें। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें स्त्रियों के गुणों के ह्रास के विषय में पढ़ा है और उसका मुख्य कारण है दया की भावना का ह्रास। दूसरे शब्दों में स्त्री का प्राकृतिक गुण देया है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने में दूसरे का ध्यान रखने की भावना, दया और सहानुभूति के गुण पैदा करने चाहिए। इन गुणों के बिना हम मानव कहलाने के योग्य नहीं हैं, बल्कि केवल नर पशु हैं और अधिक कुछ नहीं।
(4) There is famous ………………. my dear.
एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें बताती है कि संसार विष वृक्ष है। इस अपूर्ण विश्व में अर्थात् संसार में अद्वितीय गुणों के दो फल हैं। वे हैं अपनी महान् साहित्यिक कृतियों का अध्ययन और महान् विचारकों के साथ एकरूपता। यही वे दो बातें हैं जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को बदलती हैं। मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हम अपनी महान् कृतियों का अध्ययन करें, देश की उन सभी महान् कृतियों का जो हमें विरासत में प्राप्त हुई हैं। एक उपनिषद् के छोटे से कथोपकथन में एक प्रश्न किया गया है, “अच्छे जीवन का सार क्या है?” शिक्षक उत्तर देता है, “क्या तुमने उत्तर नहीं सुना?” बादलों की गड़गड़ाहट होती है–दा-दा-दा, तुरन्त शिक्षक ने समझाया कि यही अच्छे जीवन का सार है दम, दान व दया। यही अच्छे जीवन का निर्माण करती हैं। दम का अर्थ है आत्म-नियन्त्रण जो मानवता का प्रतीक है। रामायण में बताया गया है जब लक्ष्मण वन को जाने लगे तब उसकी माता ने उन्हें बताया, “राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना, सीता को अपनी माता के समान, वन को अयोध्या के समान समझना, जाओ, मेरे प्रिय बेटे।”
(5) There are ever ………………. a great nation.
हमारी साहित्यिक कृतियों में बहुत-सी ऐसी आनन्ददायक कहानियाँ हैं जो हमारे भीतर महान् नैतिक शक्ति का संचार करती हैं जो हमारे लिए ऐसी रूपरेखा बनाती हैं जिनके अनुरूप हम अपना आचरण बनाते हैं।
हमें अच्छी स्त्रियाँ दो, हमारी सभ्यता महान् होगी।
हमें अच्छी माताएँ दो, हमारा राष्ट्र महान् होगा।
(6) When you talk ………………. tatha.
जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं तब आपके सम्मुख कुछ लक्ष्य होते हैं-जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रह रहे हैं—यह ज्ञान आप विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल से प्राप्त कर सकेंगे। आप लोगों को कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित करें ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इन बातों को पूरे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है अर्थात् उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और तकनीकी योग्यता जिसके द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। किन्तु उस शिक्षा की क्या विशेषता है जो हमारे देश के विद्यालयों में दी जा रही है। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दक्षता और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उच्च जीवन की प्राप्ति का प्रयास करना है। एक ऐसे संसार के निर्माण का प्रयास जो स्थान व समय से परे हो यद्यपि बाद वाला पहले वाले को प्रकाशित तथा क्रियाशील करता है। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। सदियों तक हमने स्त्री जाति की उपेक्षा की है। परम्परा सम्भवतः इससे भिन्न रही है।
पुराकल्पेषु नारीनां मन्दिरा वन्दना निश्चितः।
अध्यापनाञ्च वेदानां गायत्री वाचानां तथा।।
(7) In ancient times ………………. into their own.
प्राचीन समय में हमारी स्त्रियों में उपनयन संस्कार होता था। वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी हो जाती थीं। वे गायत्री मन्त्र का जाप करने की भी अधिकारी हो जाती थीं। ये सभी बातें हमारी स्त्रियों के लिए खुली थीं। किन्तु हमारी सभ्यता संकुचित हो गयी और स्त्रियों की पराधीनता हमारी सभ्यता के पतन का एक प्रतीक है।
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी के अथक प्रयासों से हमारे देश में एक क्रान्ति आई और अब स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं।
Understanding the Text is
Explanations
Explain one of the following passages with reference to the context:
(1) You are living ………………. your work. [2018]
Or
Society requires ………………. disciplined mind. [2018]
Reference : These lines have been taken from the lesson ‘Women’s Education’ written by S. Radhakrishnan. [ N.B.: The above reference will be used for all explanations of this lesson.]
Context : In this lesson the author lays emphasis on the need of education for women in India. He advocates that a drastic change should be brought about in the educational pattern specially for women. He wants that the education should be according to the needs of the present time.
Explanation : In this passage the author makes it clear that we are now living in an age which is much different to the previous ages. Those were the ages when women were kept confined in the four walls of their houses. But now the women are free to come out of the houses and work in different fields of life social, public and political. They have a lot of opportunities in these fields. But they should have discipline and controlled manners. They should be honest in their dealing. Only then they will get success and pleasures.
(2) Actually in our country ………………. and bitter. [2014]
Context : In this lesson the author tells us about education particularly about girls’ education. In our country the girls’ education is not widespread. So, we should encourage every institution which contributes in spreading the girls’ education.
Explanation : In these lines the author describes the types of education he wants. There are two essentials of good education–broad education and deep education. No doubt the education given in our schools and colleges is very wide. But it is lacking in depth. We should not be satisfied only with learning and skill. But we should understand the purpose of our life. Without knowing the purpose, we shall be misguided. We shall do mistakes and our life will be painful.
(3) Therefore it is essential ………………. for yourselves. [2013, 16, 18]
Context : The author feels that our education is lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life, our lives may become blind and bitter.
Explanation : To avoid bitterness and blindness in our life, it is necessary that the education which you gain in the schools and colleges should not only add to your knowledge and technique but should also provide you with a clearly defined purpose in life. As regards the purpose, you have to outline it yourself depending upon the needs.
(4) It is said that vidya ………………. present generation. [2009, 14, 16]
Context : Here the author says that the real aim of education is to have a definite purpose of life. Education helps us in it by enabling us to decide what is right and what is wrong.
Explanation : The author tells us that vidya (knowledge) gives us wisdom and enables us to differentiate between right and wrong. So, the author advises us to find out what is needed in us in the present generation. The world is very wide and is rapidly changing. So, the purpose of life also changes in the changed conditions. One particular purpose cannot hold good in all times. So, it is our duty to decide a purpose of life carefully keeping in view the needs of the present generation. Education helps us a lot in this matter.
(5) Compassion, daya, is ……………… more than that. [2011, 16]
Context : Here, the author tells us about one of the greatest qualities of human beings, i.e., compassion. Compassion means pity including sympathy and consideration of others.
Explanation : The author says that compassion or pity is the natural quality of a woman. But it does not mean that men should not have pity. In fact compassion is the quality of every human being. It is compassion which differentiates man from animal. Every one of us should be sympathetic for others. We should be considerate of joys and sorrows of our fellow beings. Pity, sympathy and considerateness make a man civilized. So, if we want to have a strong society, we should develop these qualities in ourselves.
(6) When you talk ………………. livelihood. [2013, 18]
Context : The author has highlighted the value of good women and educated mothers for a nation.
Explanation : In these lines the author is explaining the two of the many purposes of education. The first purpose of education is to give as much theoretical knowledge to the students as we can. This is possible by teaching them science, history and geography. The other purpose of education is to teach the people to gain applied and industrial ability to do jobs by themselves. This will enable them to earn a means of living.
(7) But what is there ………………. education. [2010, 16, 17, 18]
Context : There are several aims of education. First is that education imparts us knowledge of the world in which we live. Science, history, geography and other subjects help us in this field. Second aim of education is to develop technical skill so that man may earn his livelihood.
Explanation : In these lines the author says that these are not the real aims of knowledge. Only getting information and skill are the ordinary aims. The main aim of education is to enable a man to pass a nobler and higher life. To make a man successful in this world is to enable a man to enjoy permanent bliss of spiritual life.
(8) In ancient times. ………………. subjection of women. [2010, 17]
Context : The author has told that the real aim of education should be to enable a man to pass a nobler and higher life. Here the writer tells us about the education of women in ancient times.
Explanation : In these lines the author points out that in ancient times the women had equal rights to men in the field of education. They had the right to perform all religious ceremonies. They had the right to study vedas and to sing gayatri mantra. Their status was not inferior to men in any way. But the ancient civilization began to decline and it affected the rights of women adversely.
(9) After Independence ………………. their own.
Context : The author is narrating the position and role of women in our country. In ancient times they occupied a valuable position but in time to follow they became subdued.
Explanation : The writer says that after India became free on account of the relentless efforts of Gandhiji, a welcome change has been brought out in the condition of women in our country. Women are now receiving their old heritage and regaining their valuable position.
Short Answer Type Questions
Answer one of the following questions in not more than 30 words:
Question 1.
What are the opportunities available to women in our times ? [2013, 15]
(हमारे समय में स्त्रियों को कौन-से अवसर उपलब्ध हैं?)
Answer :
In our times there are opportunities for women in social work, public life and administration.
(हमारे समय में स्त्रियों को सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में तथा प्रशासन में बड़े अवसर उपलब्ध
Question 2.
What kind of women does the society need ? [2017, 18]
(समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है?)
Or
What qualities should the women have according to the present needs of the society?
(आज के समाज की आवश्यकता के अनुसार स्त्रियों में क्या गुण होने चाहिए ?)
Answer :
Society needs disciplined women of controlled behaviour.
(समाज को नियन्त्रित व्यवहार वाली अनुशासित स्त्रियाँ चाहिए।)
Question 3.
What is the real.situation regarding women’s education in India ?
(भारत में स्त्रियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है?)
Answer :
In reality women’s education in India is not wide spread.
(वास्तव में भारतवर्ष में स्त्रियों की शिक्षा विस्तृत रूप से फैली हुई नहीं है।)
Question 4.
What kind of education does the author recommend (or advocate) and why?
(लेखक किस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश करता है और क्यों?).
Answer :
The author recommends an education with a definite purpose because education without purpose leads towards mistaken deeds resulting in grief.
(लेखक निश्चित उद्देश्य वाली शिक्षा की सिफारिश करता है, क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है जिसके परिणामस्वरूप दुःख होता है।)
Question 5.
Point out the difference between the cultured and the uncultured mind so far as attitude towards life is concerned.
(जहा तक जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सम्बन्ध है सुसंस्कृत तथा असंस्कृत मस्तिष्क का अन्तर स्पष्ट करो।)
Answer :
A cultured mind is dedicated to a single purpose while uncultured mind is scattered in many directions.
(एक सुसंस्कृत मस्तिष्क एक ही लक्ष्य की ओर लगा रहता है, जबकि असंस्कृत मस्तिष्क भिन्न-भिन्न दिशाओं में बिखरा रहता है।)
Question 6.
Which particular quality distinguishes men from women ? [2009, 17]
(कौन-सी विशेष गुण पुरुषों को स्त्रियों से भिन्न करता है?)
Answer :
Compassion or feeling of pity distinguishes men from women.
(दया की भावना पुरुषों को स्त्रियों से भिन्न करती है।)
Question 7.
What qualities are necessary for the development of human beings ?
(मनुष्य के विकास के लिए कौन-कौन-से गुण आवश्यक हैं?)
Answer :
Kindness, considerateness and compassion are necessary qualities for the development of human beings.
(दया, दूसरों के प्रति विचारशील होना तथा सहानुभूति मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक गुण हैं।)
Question 8.
What are the two important products of the tree of life and what is their effect on human beings ?
(जीवन-रूपी वृक्ष के दो मुख्य उत्पाद क्या हैं और मनुष्य पर उनका क्या प्रभाव होता है ?)
Answer :
The two important products of the tree of life are—the study of our ancient literature and communion with great minds. These two things mould men’s mind and heart.
(जीवन-रूपी वृक्ष के दो प्रमुख उत्पाद हैं—अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन और महान् व्यक्तियों से मस्तिष्क द्वारा सम्पर्क। ये दो वस्तुएँ मनुष्यों के मस्तिष्कों और हृदयों को बदल देती हैं।)
Question 9.
What are the three important qualities of a valuable life? [2018]
(सारयुक्त जीवन के तीन महत्त्वपूर्ण गुण कौन-कौन से हैं?)
Or
What constitutes the essence of good life ? [2017]
(जीवन का सार कौन-सी बात बनाती है?)
Answer :
The three important qualities of a valuable life are—Dama i.e. self-control, Dana i.e. charity and Daya i.e. compassion.
(सारयुक्त जीवन के तीन मुख्य गुण हैं—दम अर्थात् आत्म-नियन्त्रण, दान अर्थात् सहायता और दया अर्थात् सहानुभूति।)
Question 10.
What aims do people have in view generally when they talk about : education ?
(जब लोग शिक्षा के विषय में बात करते हैं, तब सामान्यत: उनके विचार से शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं?)
Answer :
Generally the people have two aims of education in their view—
(i) to give the student knowledge of the world in which they live through science, history and geography,
(ii) to give them technical skill to earn their livelihood.
(साधारणत: लोगों के मन में शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं–
(i) विद्यार्थियों को विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल के द्वारा उस संसार का ज्ञान देना जिसमें वे रहते हैं,
(ii) उन्हें तकनीकी कुशलता देना ताकि वे अपनी : आजीविका प्राप्त कर सकें।)
Question 11.
State the chief purpose of education. [2013, 18]
(शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए।)।
Answer :
The chief purpose of education is not merely to gain skill or to know more and more about the world but the chief purpose of education is the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time.
(शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कार्य-निपुणता प्राप्त करना अथवा संसार की अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च जीवन को जानने का प्रयास करना है, उस संसार को जानने का प्रयास करना है जो स्थान और समय से कहीं ऊपर हो।)
Question 12.
What were the things women entitled to in ancient India ? [2018]
(वे कौन-कौन सी बातें थीं जिनका प्राचीन भारत में स्त्रियों को अधिकार था?)
Answer :
In ancient India women were entitled to study Vedas and to the chanting of Gayatri mantra.
(प्राचीन भारत में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने तथा गायत्री मन्त्र का जप करने का अधिकार था।)
Question 13.
What is one of the signs of the decline of our civilization ?
(हमारी सभ्यता के पतन का एक चिह्न क्या है ?)
Answer :
Subjection of women is one of the signs of the decline of our civilization.
(स्त्रियों की पराधीनता हमारी सभ्यता के पतन का एक चिह्न है।)
Question 14.
Through whose efforts has a change been brought about in the condition of women after Independence ?
(स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियों की दशा में परिवर्तन किसके प्रयासों से आया?)
Answer :
Through the efforts of Mahatma Gandhi, a change has been brought about in the condition of women after independence.
(स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी के प्रयासों से स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आया है।)
Question 15.
Briefly describe the importance of the study of classics in shaping the personality of men and women in society.
(हमारे समाज में पुरुष और स्त्रियों के व्यक्तित्व को बनाने में प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।)
Answer :
When we study our classics, we come in close contact of different characters and minds. There we find many examples which fill us with the feelings of considerateness, kindness and compassion which shape the personality of men and women in our society.
(जब हम अपने प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं तब हम भिन्न-भिन्न चरित्रों एवं विद्वानों के सम्पर्क में आते हैं। वहाँ हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें दूसरों के प्रति विचारवान बनाते हैं तथा दया और सहानुभूति की भावनाओं से भर देते हैं जो हमारे समाज में स्त्री तथा पुरुषों के व्यक्तित्व को बनाती है।)
Question 16.
Why is education of women essential for a nation ?
(किसी राष्ट्र की स्त्रियों के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है?)
Answer :
The progress of nation depends upon its women also. So, the education of women is essential so that they may be broad minded and well disciplined.
(किसी राष्ट्र की उन्नति उसकी स्त्रियों पर भी निर्भर करती है। इसीलिए स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है ताकि वे विशाल मस्तिष्क वाली तथा अनुशासित हों।)
Question 17.
What was the great teaching that Lakshman’s mother gave him when he was going to the forest ? [2011, 18]
(लक्ष्मण की माता ने उसे क्या महान् शिक्षा दी जब वे जंगल को जा रहे थे ?)
Answer :
When Lakshman was going to the forest, his mother taught him, “Look upon, Ram as your father, look upon Sita as myself, look upon the forest as Ayodhya.” (जब लक्ष्मण वन को जाने लगे तब उनकी माता ने उन्हें सिखाया, “राम को अपने पिता के समान, सीता को अपनी माता के समान और वन को अयोध्या के समान समझना।)
Question 18.
What causes the decline of womanhood, according to S. Radhakrishnan? [2013,15]
(एस० राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के पतन का क्या कारण है?)
Answer :
According to S. Radhakrishnan, subjection of women causes the decline of womanhood. (एस० राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के पतन का कारण नारी की पराधीनता है।)
Vocabulary
Choose the most appropriate word or phrase that best completes the sentence:
1. Society requires women of disciplined minds and ……………… manners. [2017]
(a) controlled
(b) restrained
(c) good
(d) disciplined
2. Actually in our country, education, ……………… girl’s education is concerned, is not widespread enough.
(a) so far as
(b) as far as
(c) so long as
(d) as long as
3. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be ……………… [2017]
(a) meaningful
(b) useful
(c) purposeful
(d) deep
4. So the purpose which you ……………… in your life must he adapted to the relevant needs of the present generation.
(a) accept
(b) recognise
(c) adapt
(d) adopt
5. I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the ………………
(a) master
(b) possessor
(c) upholders
(d) inheritors
6. There are ever so many ……………… stories in our classics which will in still into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves.
(a) thrilling
(b) joyful
(c) inspiring
(d) moral
7. But our civilization became arrested and one of the main signs of that ……… of our civilization is the subjection of women.
(a) fall
(b) ruin
(c) set back
(d) decay
8. After Independence, through the exertions of ……………… a revolution has been effected in our country, and women are coming into their own.
(a) Mahatma Gandhi
(b) Vinoba Bhave
(c) Mother Teresa
(d) Jawaharlal Nehru
9. When you talk about education, you have several aims ………………
(a) openly
(b) in view
(c) internally
(d) out of tune
10. For some ……………… We neglected our women folk. [2017]
(a) years
(b) weeks
(c) decades
(d) centuries
11. If you do not have ……………… you are not human. [2017]
(a) power
(b) compassion
(c) glory
(d) money
12. You are living in an age when there are great ……………… for women in social work. [2017]
(a) profits
(b) problems
(c) opportunities
(d) dangers
13. The natural quality of women is ……………… [2018]
(a) indifference
(b) charm
(c) selfishness
(d) compassion
14. ……………… is the quality which is more characteristic of women than men. [2012, 18].
(a) Emotion
(b) Compassion
(c) Passion
(d) Impassioned
15. When you talk about education, you have ……………… aims in view. [2016]
(a) several
(b) plenty of
(c) so many
(d) a number of
16. We have heard that the chief ……………… of education is not merely the acquiring of skill or information but the initiation into a higher life. [2016]
(a) aim
(b) goal
(c) purpose
(d) principle
Answers :
1. (b), 2. (b), 3. (b), 4. (d), 5. (), 6. (a), 7. (d), 8. (a), 9. (b), 10. (d), 11. (b), 12. (c), 13. (d), 14. (b), 15. (a), 16. (c).
We hope the UP Board Solutions for Class 12 English Prose Chapter 6 Women’s Education help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 English Prose Chapter 6 Women’s Education, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.