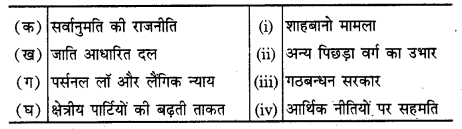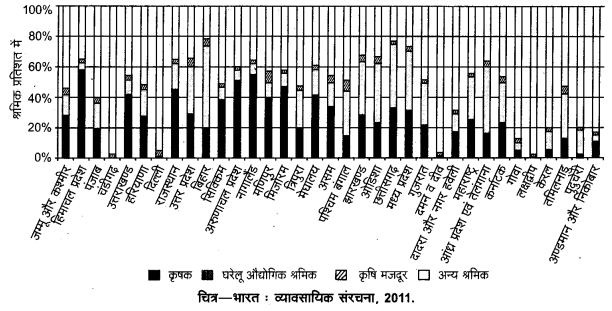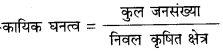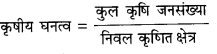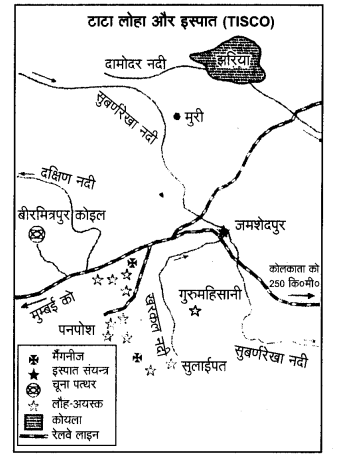UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 2 Migration: Types, Causes and Consequences (प्रवास-प्रकार, कारण और परिणाम)
UP Board Class 12 Geography Chapter 2 Text Book Questions
UP Board Class 12 Geography Chapter 2 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1.
नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
(i) निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है
(क) विवाह
(ख) व्यवसाय
(ग) काम और रोजगार
(घ) विवाह।
उत्तर:
(ग) काम और रोजगार।
(ii) निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं
(क) उत्तर प्रदेश
(ख) दिल्ली
(ग) महाराष्ट्र
(घ) बिहार।
उत्तर:
(ग) महाराष्ट्र।
(iii) भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी एक धारा पुरुष प्रधान है
(क) ग्रामीण से ग्रामीण
(ख) नगरीय से ग्रामीण
(ग) ग्रामीण से नगरीय
(घ) नगरीय से नगरीय।
उत्तर:
(ग) ग्रामीण से नगरीय।
(iv) निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है—
(क) मुम्बई नगरीय समूहन
(ख) दिल्ली नगरीय समूहन
(ग) बंगलुरु नगरीय समूहन
(घ) चेन्नई नगरीय समूहन।
उत्तर:
(क) मुम्बई नगरीय समूहन।
![]()
प्रश्न 2.
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें
(i) जीवनपर्यन्त प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
जीवनपर्यन्त प्रवास – यह वह प्रवास होता है जो जन्म के स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। इसे ‘जीवनपर्यन्त प्रवास’ के नाम से जाना जाता है।
पिछले स्थान प्रवास – इसमें निवास का स्थान पिछले निवास से भिन्न होता है। इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाता है।
(ii) पुरुष/स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए।
उत्तर:
पुरुष बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से नगरों की तरफ रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। स्त्रियाँ विवाह के कारण प्रवास करती हैं। भारत में प्रत्येक लड़की को विवाह के बाद अपने मायके के घर से ससुराल के घर तक प्रवास करना होता है।
(iii) उद्गम और गन्तव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण-नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
बड़ी संख्या में युवक रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों की संख्या में कमी हो जाती है और नगरों में उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। गाँवों में वृद्ध, बच्चे और स्त्रियाँ रह जाती हैं, अत: ग्रामीण-नगरीय प्रवास से उद्गम तथा गन्तव्य दोनों ही स्थानों की आयु एवं लिंग संरचना पर प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न 3.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें
(i) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए।
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास – जब किसी देश-विशेष का निवासी किन्हीं विशेष कारणों से अन्य देश में प्रवासित हो जाता है तो उसे ‘अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास’ कहते हैं।
भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
1. आर्थिक कारण – भारत में संसाधनों का भण्डार है। यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास में इन संसाधनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। भारत में प्रवासी इन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से अधिक आते हैं। वर्तमान में अनेक विदेशी कम्पनियाँ भारत में इसी आकर्षण के कारण स्थापित हुई हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने उत्पादों के लिए कच्चा माल, सस्ता श्रम और व्यापक बाजार आदि सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
2. राजनीतिक कारण – भारत में राजनीतिक कारणों या सरकारी नीतियों के लचीलेपन के कारण भी विदेशी प्रवास करते हैं। सीमावर्ती देशों से होने वाला प्रवास इसका उदाहरण है।
3. धार्मिक और सामाजिक कारण – भारत सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम् सिद्धान्त एवं आदि संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्पन्नता आदि से प्रभावित होकर और समाज में सहायता से समन्वय के कारण प्रवासी आकर्षित होते हैं जिसके कारण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास होता है।
इस तरह भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हैं. किन्तु वर्तमान समय में अनेक अन्य कारणों; जैसे-तकनीकी सुविधाओं, उच्च प्रतिभा तथा उच्च शिक्षा आदि से भी भारत के लोग खाड़ी देशों एवं यू०एस०ए० और यूरोपीय देशों को प्रवास करते हैं।
(ii) प्रवास के सामाजिक जनांकिकीय परिणाम क्या-क्या हैं?
उत्तर:
प्रवास के सामाजिक परिणाम
- नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार कल्याण, बालिका शिक्षा आदि नए विचारों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होता है।
- विविध संस्कृतियों का अन्त:मिश्रण होता है।
- प्रवास लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं में फँसा देता है।
प्रवास के जनांकिकीय परिणाम
- प्रवास से आयु लिंगानुपात में असन्तुलन उत्पन्न होता है।
- नगरों में लिंगानुपात घट जाता है तथा युवा वर्ग श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है तथा कुशल युवा श्रमिकों का अनुपात घट जाता है।
UP Board Class 12 Geography Chapter 2 Other Important Questions
UP Board Class 12 Geography Chapter 2 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
प्रवास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
प्रवास के प्रमुख कारण प्रवास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
1. आजीविका – सीमित कृषि भूमि और बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में एक निश्चित जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। कुटीर उद्योगों की पतली हालत और कृषि में बढ़ते . मशीनीकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग को गाँवों में आजीविका नहीं मिल पाती। गाँवों में ये बेरोजगार अधिशेष जनसंख्या के रूप में नगरों में रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक सम्भावनाएँ होती हैं।
2. विवाह – सामाजिक रीति-रिवाजों के अन्तर्गत विवाह के उपरान्त लड़कियों को माता-पिता का घर छोड़कर ससुराल जाकर रहना होता है। भारत में इसी कारण स्त्रियों के प्रवास की संख्या उच्च है।
3. शिक्षा और वृत्तिका – योग्यता की वृद्धि हेतु लोग शहरों में विभिन्न प्रकार की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में प्रवास करते हैं। अपनी वृत्तिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए भी सुनिश्चित, निपुण व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा किसी भी क्षेत्र में योग्य व्यक्ति शहरों में उन्नति के अवसर तलाशते हैं।
4. सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप – राजनीतिक अस्थिरता एवं गड़बड़ी, जातीय दंगे, देश-विभाजन, वर्ग-संघर्ष से त्रस्त होकर लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ प्रवास करते हैं। अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप भी जनसंख्या को प्रवास करने के लिए बाधित करते हैं; जैसे—बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकम्प, सुनामी आदि।
![]()
प्रश्न 2.
प्रवास के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
प्रवास के आर्थिक परिणाम प्रवासी उद्गम प्रदेश में स्थित अपने घरों को कमाई का पैसा भेजते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशियाँ विदेशी-विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आन्तरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि काफी कम है, किन्तु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस राशि का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश, गृह-निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गाँवों की अर्थव्यवस्था के लिए यह राशि शरीर में धमनियों की तरह कार्य करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए, उसकी हरित क्रान्ति कार्ययोजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर अकुशल प्रवासियों के प्रवास के प्रमुख कारण बताइए।
उत्तर:
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर अकुशल प्रवासियों के प्रवास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
- इसका सबसे प्रमुख कारण निर्धनता है।
- नगरों में श्रमिकों की माँग प्रायः अधिक रहती है।
- नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम तथा वेतनमान निम्न होता है।
प्रश्न 2.
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर अकुशल प्रवासियों के प्रवास के कष्टों को समझाइए।
उत्तर:
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर अकुशल प्रवासियों के प्रवास के कष्ट निम्नलिखित
- नगरीय क्षेत्रों में मजबूरन कम वेतन पर नौकरी करना।
- परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति व्याकुलता उत्पन्न करती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों के प्रवास के कारण परिवार पीछे छूट जाता है, जिससे परिवार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
- प्रवास से विविध संस्कृतियों का मिश्रण होता है। इससे गुमनामी जैसे नकारात्मक परिणाम भी होते हैं।
प्रश्न 3.
प्रवास के अपकर्ष व प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
जनसंख्या प्रवास को अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं
1. अपकर्ष कारक-जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो यह ‘अपकर्ष प्रेरित प्रवास’ कहलाता है।
2. प्रतिकर्ष कारक-जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व अन्य सुविधाओं की कमी अथवा गरीबी और भुखमरी के कारण मजबूरी में गाँव छोड़कर शहर में जा बसते हैं तो इसे ‘प्रतिकर्ष प्रेरित प्रवास’ कहते हैं।
![]()
प्रश्न 4.
दिक् परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
नगरों तथा गाँवों से शहरों के बीच जनसंख्या के दैनिक स्थानान्तरण को ‘दिक परिवर्तन’ कहते हैं। यह केवल दैनिक होता है।
प्रश्न 5.
भारत में प्रवास के परिणामों को समझाइए।
उत्तर:
भारत में प्रवास के परिणाम निम्नलिखित हैं
- प्रवास के कारण क्षेत्र-विशेष में जनसंख्या बढ़ती है; इसलिए आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- प्रवासी लोगों को रोजगार चाहिए; इसलिए रोजगार के साधनों का अभाव हो जाता है।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवहन साधनों की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- अधिक जनसंख्या के कारण स्वच्छता की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
प्रश्न 6.
उत्प्रवास के लिए उत्तरदायी प्रतिकर्ष कारकों को समझाइए।
उत्तर:
उत्प्रवास के लिए उत्तरदायी प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित हैं
- गरीबी – गरीबी के कारण जनसंख्या उन स्थानों को प्रवास करती है जहाँ पर उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।
- शिक्षा – शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण अधिक शिक्षा लेने के लिए लोग उत्प्रवास करते हैं।
- जनसंख्या का अधिक दबाव – जनसंख्या के अधिक दबाव से बच्चे के लिए लोग अन्य स्थानों पर जहाँ जनसंख्या कम होती है, प्रवास करते हैं।
- सुरक्षा – सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग सुरक्षित स्थानों को प्रवास करते हैं। .
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
प्रवास का क्या अर्थ है?
उत्तर:
प्रवास’ का अर्थ जनसंख्या का उद्गम स्थान से गन्तव्य की ओर गमन है।
प्रश्न 2.
उत्प्रवास किसे कहते हैं?
उत्तर:
जब एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो यह ‘उत्प्रवास’ कहलाता है।
प्रश्न 3.
आप्रवास किसे कहते हैं?
उत्तर:
यदि व्यक्ति अन्य स्थानों से आकर एक विशिष्ट स्थान पर बस जाता है, तो यह ‘आप्रवास’ कहलाता है।
प्रश्न 4.
आन्तरिक प्रवास से क्या आशय है? .
उत्तर:
आन्तरिक प्रवास में लोगों का पलायन मुख्य रूप से देश की राजनीतिक सीमाओं के अन्दर ही होता है। उदाहरण के लिए; बिहार के लोगों का उत्तर प्रदेश में प्रवास।
प्रश्न 5.
अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या आशय है?
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास में लोग राजनीतिक सीमाओं (देश) से बाहर पलायन कर जाते हैं। उदाहरण के लिए; राजस्थान के लोगों का यू०के० तथा कनाडा में प्रवास।
प्रश्न 6
भारत में आन्तरिक प्रवास के कितने प्रवाह हैं? नाम लिखिए।
उत्तर:
भारत में आन्तरिक प्रवास के चार प्रवाह हैं
- ग्रामीण से ग्रामीण
- ग्रामीण से नगरीय
- नगरीय से नगरीय, तथा
- नगरीय से ग्रामीण।
![]()
प्रश्न 7.
प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए।
उत्तर:
प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम हैं
- नगरों की अनियोजित वृद्धि
- गन्दी बस्तियाँ
- विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, तथा
- अपशिष्ट निपटान की समस्या आदि।
प्रश्न 8.
अन्तर्राज्यीय प्रवास से क्या आशय है?
उत्तर:
लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अन्तर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, जैसे—अम्बाला से मेरठ प्रवास को जाना।
प्रश्न 9.
अन्तःराज्यीय प्रवास से क्या आशय है?
उत्तर:
लोगों का एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अन्तःराज्यीय प्रवास कहलाता है, जैसे-आगरा से मेरठ प्रवास को जाना।
प्रश्न 10.
प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक बताइए।
उत्तर:
प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक है
- बेहतर सुविधाएँ
- सुरक्षा
- नागरिक सुविधाएँ, तथा
- स्वास्थ्य सुविधाएँ।
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
स्थानान्तरण की दिशा के आधार पर आन्तरिक प्रवास की कितनी धाराओं की पहचान की गई
(a) तीन
(b) चार
(c) पाँच .
(d) छह।
उत्तर:
(b) चार।
प्रश्न 2.
प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है
(a) शिक्षा
(b) मनोरंजन
(c) रोजगार
(d) उपर्युक्त संभी।
उत्तर:
(d) उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 3.
प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक है
(a) आजीविका
(b) विवाह
(c) शिक्षा और वृत्तिका
(d) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
(d) उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 4.
यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे कहते हैं
(a) अन्त:राज्यीय प्रवास
(b) अन्तर्राज्यीय प्रवास
(c) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास
(d) उत्प्रवास।
उत्तर:
(b) अन्तर्राज्यीय प्रवास।
प्रश्न 5.
प्रवास होता है
(a) नगर से नगर को
(b) ग्राम से नगर को
(c) ग्राम से ग्राम को
(d) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
(d) उपर्युक्त सभी।
![]()
प्रश्न 6.
कौन-सा कारण प्रतिकर्ष का कारक नहीं है
(a) मनोरंजन
(b) गरीबी
(c) जनसंख्या दबाव
(d) आपदा।
उत्तर:
(c) जनसंख्या दबाव।
प्रश्न 7.
सामाजिक प्रवास के कितने रूप हैं
(a) दो
(b) तीन
(c) चार
(d) पाँच।
उत्तर:
(a) दो।
प्रश्न 8.
किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है
(a) केरल
(b) कर्नाटक
(c) बिहार
(d) मेघालय।
उत्तर:
(d) मेघालय।