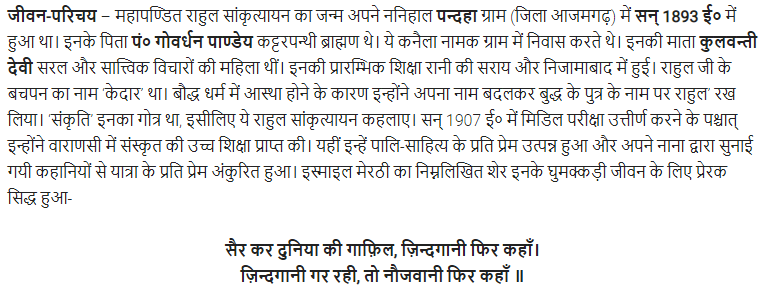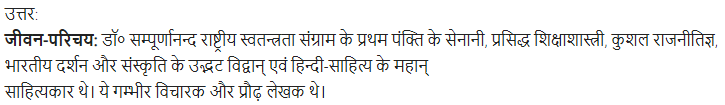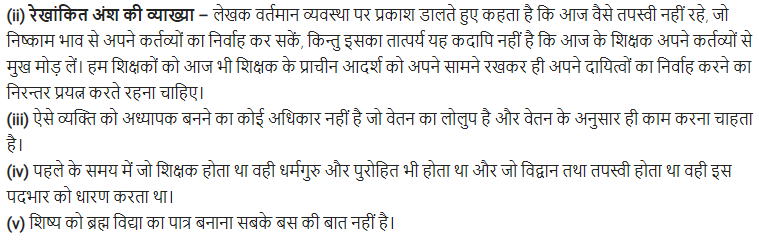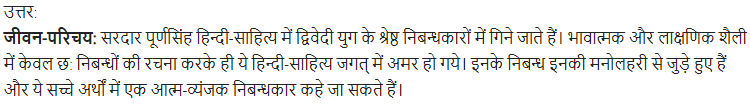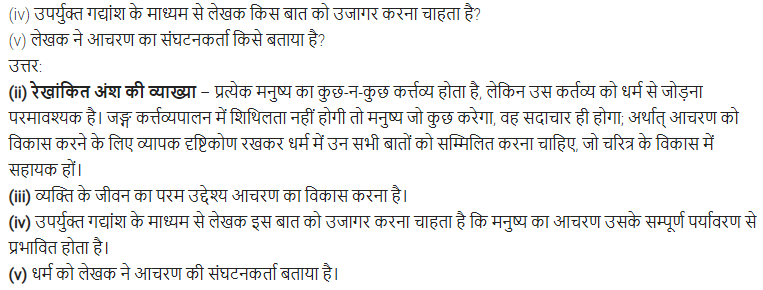UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 10 State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में) are the part of UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 10 State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 11 |
| Subject | Pedagogy |
| Chapter | Chapter 10 |
| Chapter Name | State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में) |
| Number of Questions | 15 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 10 State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में)
वस्तुत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
राज्य से आप क्या समझते हैं? राज्य के मुख्य शैक्षिक कार्यों का उल्लेख कीजिए।
शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए।
या
राज्य के शैक्षिक कार्यों का वर्णन कीजिए।
या
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के उत्तर:दायित्वों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
राज्य की परिभाषा
राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित भूमि पर रहता है, जिसकी अपनी संगठित सरकार होती है और जो बाह्य नियन्त्रणों से पूर्ण स्वतन्त्र होती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि राज्य के चार तत्त्व होते हैं-भूमि या प्रदेश, जनसंख्या, सरकार एवं सम्प्रभुता।
राज्य की परिभाषा देते हुए गार्नर ने लिखा है, “राज्य न्यून संख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों के समुदाय को कहते हैं जो कि निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाहरी नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त है और जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार होती है, जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश निवासी स्वाभाविक रूप से करते हैं।’
राज्य के शैक्षिक कार्य
राज्य के शैक्षिक कार्यों का विवेचन निम्नलिखित है
1. राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण-राज्य का सबसे पहला कार्य यह है कि वह देश में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा योजना का संचालन करे, जिससे समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा हो सके। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर राज्य शिक्षाशास्त्रियों, विचारकों एवं राजनीतिज्ञों के सहयोग से एक शिक्षा योजना बनाता है और उसके द्वारा नागरिकों के सर्वांगीण विकास का। प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं माध्यम को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना का वास्तविक जीवन के निकट होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो सके।
2. शिक्षा को अनिवार्य करना-राज्य को राष्ट्र के सभी बालकों के बौद्धिक और मानसिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विकास होने पर ही वह इसे योग्य बन सकेंगे कि अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझ सकें। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाए। इससे देश के सभी नागरिक शिक्षित होंगे और वे अपना तथा देश का कल्याण कर सकेंगे।
3. विद्यालयों की स्थापना-वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करे और व्यक्तिगत प्रयासों से खुले हुए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करे। राज्य को विद्यालयों के निरीक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
4. शिक्षा हेतु धन का प्रबन्ध-राज्य का यह एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह सभी स्तरों की शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करे। इसके साथ-ही-साथ राज्य को सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। राज्य सरकारी विद्यालयों के व्यय का वहन तो करेगा ही, लेकिन गैर-सरकारी विद्यालयों को भी उसे अनुदान देना चाहिए।
5. योग्य शिक्षकों की व्यवस्था-शिक्षा प्रक्रिया को समुचित रूप से चलाने के लिए कुशल एवं योग्य शिक्षकों की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यार्थियों के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्थान-स्थान पर प्रशिक्षण विद्यालय खोलता है, जो देश के लिए योग्य शिक्षक तैयार करते हैं। इसके साथ-ही-साथ राज्य यह भी व्यवस्था करता है कि प्रशिक्षित अध्यापकों को उनकी योग्यतानुसार विद्यालयों में अध्यापन कार्य का अवसर मिले, ताकि देश की शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ सके।
6. सैनिक शिक्षा की व्यवस्था-उच्च विद्यालयों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश के नवयुवक बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा कर सकें। इसके लिए राज्य की ओर से स्थान-स्थान पर सैनिक विद्यालयों की स्थापना की जाती है।
7. नागरिकता का प्रशिक्षण-लोकतन्त्र की प्रगति एवं स्थायित्व योग्य नागरिकों पर निर्भर है। अतः राज्य का कार्य बालकों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना है, जिससे वह नागरिक गुणों से सुसज्जित होकर राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास में योगदान दे सके। प्रशिक्षण चार रूपों में होना चाहिए
- राजनीतिक प्रशिक्षण- राज्य को चाहिए कि वह नवयुवकों के मन में अपनी राजनीतिक विचारधारा को समाविष्ट कर दे। इसके लिए उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे नागरिक यह समझने लगेंगे कि उनके कर्तव्य और अधिकार क्या हैं और उनका पालन किस प्रकार करना चाहिए। वह राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय भाग ले सकेंगे। इसके लिए राज्य को रेडियो प्रसारण, राजनीतिक प्रदर्शनी, राजनीतिक उत्सवों आदि का आयोजन करना चाहिए।
- सामाजिक प्रशिक्षण- राज्य को छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वह समाज के महत्त्वपूर्ण सदस्य बन सकें। राज्य को इस प्रकार का सामाजिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें रहकर सामाजिक भावना का विकास हो और व्यक्ति समाज की प्रगति के लिए कार्य करे।
- आर्थिक प्रशिक्षण- किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को आर्थिक दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वह कृषि, उद्योग, विज्ञान आदि के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करे, जिससे कि नवयुवक जीविकोपार्जन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- सांस्कृतिक प्रशिक्षण- राज्य को चाहिए कि वह देश के नवयुवकों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्रदान करे, जिससे कि वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा तथा उसका विकास कर सकें। इसके लिए राज्य को स्थान-स्थान पर सांस्कृतिक सोसाइटियों, चित्रशालाओं, अजायबघरों, मनोरंजन गृहों इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ-ही-साथ राज्य को चाहिए कि वह सांस्कृतिक मण्डलों, सांस्कृतिक भ्रमणों एवं सामुदायिक केन्द्रों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करे।
8. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण-राज्य का कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता देना है। इसके लिए राज्य के उच्चकोटि के दार्शनिकों, शिक्षा विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों व शिक्षा मन्त्रियों को समाज की आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए और फिर इन आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए।
9. परिवार और विद्यालयों में सम्बन्ध स्थापित करना- राज्य को एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि अभिभावकों एवं शिक्षकों के प्रतिनिधि और उच्चकोटि के शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हों। इस संस्था का कार्य यह विचार करना है कि किस तरह से शिक्षा द्वारा व्यक्ति और समाज का हित सम्भव हो सकता है।
10. शैक्षणिक शोध को प्रोत्साहन- शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। इन अन्वेषणों के लिए राज्य को धन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे शिक्षा के नए-नए आदर्श एवं नई-नई विधियाँ निर्मित हो सकें।
11. शिक्षण-संस्थाओं पर आवश्यक नियन्त्रण-प्रायः यह देखने में आता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी अनैतिक कार्य करते हैं, जिससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षण संस्थाओं पर आवश्यक नियन्त्रण रखे, जिससे इन शिक्षण संस्थाओं का विघटन न होने पाए। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य को अनेक प्रकार के शैक्षिक कार्य करने पड़ते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण एक बुराई है।
उत्तर:
शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण : एक बुराई
शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण हो या शिक्षा राज्य के नियन्त्रण से मुक्त हो, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य का कार्य केवल नागरिकों की रक्षा करना है। लॉक (Locke), मिल (Mill), बेन्थम (Benthem) आदि विचारकों ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। व्यक्तिवादियों का कथन है कि यद्यपि कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यक्ति राज्य का अनुशासन स्वीकार करेगा, परन्तु बहुत-से ऐसे कार्य भी हैं जिनमें व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र है। मिल का कहना है कि “व्यक्ति पवित्र है और उसकी स्वतन्त्रता में राज्य का सहसा हस्तक्षेप सहन नहीं किया जा सकता।”
इस मत के समर्थकों का तर्क है–
- राज्य का शिक्षा पर नियन्त्रण रहने से व्यक्तियों में स्वतन्त्र विचारों का प्रसार रुक जाता है और धीरे-धीरे वाणी की स्वतन्त्रता का लोप हो जाता है।
- राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा-व्यवस्था में बालक के व्यक्तिव के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी रुचियों, सीमाओं और इच्छाओं की पूर्ण अवहेलनी की जाती है और उसे राज्य द्वारा निर्धारित एक निश्चित साँचे के अनुसार अपने को ढालना होता है। प्रश्न 2 स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है।
शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है।
कुछ विद्वान् शिक्षा पर राज्य के नियन्त्रण को अच्छी बताते हैं। इनका मत है कि शिक्षित व्यक्तियों का उपयोग राज्य को ही करना है। शिक्षा पा लेने पर व्यक्ति सुयोग्य नागरिक के रूप में समाज और राज्य की सेवा में जुटेगा। इस सेवा के रूप का निर्धारण करना राज्य का कर्तव्य है। इसलिए राज्य यह अधिक अच्छी तरह समझ सकता है कि शिक्षित व्यक्तियों का उपयोग किस क्षेत्र में और कैसे किया जाए। यदि शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण के समर्थकों का यह तर्क ठीक है तो वस्तुतः राज्य को यह अधिकार है कि वह बालक की शिक्षा के रूप का निर्धारण करे।
इस मत के समर्थकों का यह भी कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयत्नों को प्रोत्साहन नहीं देना। चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत संस्थाएँ बालकों के हित को सर्वोपरि न रखकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपना काम करती हैं। इनमें अध्यापकों का वेतन बहुत कम होता है और आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध नहीं रहते। इस प्रकार समष्टिवादी मत के अनुसार शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था राज्य द्वारा ही होनी चाहिए। राज्य को शिक्षा पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। रूस के साम्यवादी विचारक पिंकविच (Pinckvitch) ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है, “सार्वजनिक शिक्षा, जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, एक ऐसा शक्तिशाली यन्त्र है जो राज्य दूसरों को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।
प्रश्न 3.
बालक की शिक्षा में राज्य का अधिक महत्त्व है अथवा समाज का? इस प्रकरण पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
बालक की शिक्षा में राज्य तथा समाज का महत्त्व
बालक की शिक्षा में राज्य तथा समाज दोनों का ही विशेष योगदान तथा महत्त्व होता है। राज्य द्वारा शिक्षा की नीतियों का निर्धारण किया जाता है, शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की जाती है तथा उनकी व्यवस्था एवं संचालन किया जाता है। शिक्षा के स्तर का निर्धारण तथा शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण का कार्य भी राज्य द्वारा ही किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे भिन्न बालक के समाजीकरण तथा सद्गुणों के विकास में समाज की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है।
बालक की अनौपचारिक शिक्षा का एक मुख्य अभिकरण समाज ही है। समाज द्वारा बालक को आजीवन शिक्षित किया जाता है, जब कि राज्य द्वारा की गई शिक्षा की व्यवस्था केवल सीमित समय के लिए ही होती है। राज्य द्वारा प्रदान की गई शिक्षा प्राप्त करके बालक जीविका-उपार्जन के लिए योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है, जब कि समाज द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को प्राप्त करके बालक व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालक की औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का महत्त्व अधिक है, जब कि बालक की अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में समाज का महत्त्व अधिक है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
राज्य और शिक्षा के सम्बन्ध के विषय में समन्वयवादी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
आधुनिक शिक्षाशास्त्री न तो पूर्णरूप से व्यक्तिवादी मत को स्वीकार करते हैं और न ही समष्टिवादी मत को, बल्कि उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया है। उनके अनुसार शिक्षा को न तो राज्य के पूर्ण नियन्त्रण में रखा जा सकता है और न ही उसे राज्य के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त किया जा सकता है। उनका कथन है कि शिक्षा जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई भी एक संस्था सभी के लिए इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती। इसलिए शिक्षा पर राज्य के नियन्त्रण के साथ-साथ परिवार एवं धार्मिक संस्थाओं का भी नियन्त्रण होना चाहिए। इस प्रकार हमें राज्य के सीमित हस्तक्षेप तथा सीमित नियन्त्रण की नीति अपनानी चाहिए। राज्य का सीमित हस्तक्षेप केवल मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए।
प्रश्न 2.
स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने का कार्य केवल राज्य ही कर सकता है।
उत्तर:
शिक्षा एक सार्वजनिक रूप से सम्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। देश के सभी क्षेत्रों में बालक-बालिकाओं की शिक्षा का प्रावधान है। इस स्थिति में आवश्यक है कि शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता हो। शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने का कार्य राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। यदि शिक्षा को राज्य के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाए तो शिक्षा को संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाएँ अपने-अपने दृष्टिकोण से शिक्षा को भिन्न-भिन्न स्वरूप प्रदान कर सकती हैं, परन्तु यदि शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में होगी तो देश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा का स्वरूप एक ही होगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता होगी।
निश्चित उत्तरीय प्रत
प्रश्न 1.
‘राज्य’ की एक सरल परिभाषा लिखिए।
उत्तर:
“राज्य एक संगठन है, जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमों के द्वारा व्यवस्था बनाए रखता है।” -मैकाइवर
प्रश्न 2.
एक व्यवस्थित संगठन के रूप में राज्य के अनिवार्य तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
एक व्यवस्थित संगठन के रूप में राज्य के अनिवार्य तत्त्व हैं—
- भूमि,
- जनसंख्या,
- सरकार तथा
- सत्ता।
प्रश्न 3.
बालकों की शिक्षा के दृष्टिकोण से राज्य का मुख्यतम शैक्षिक कार्य क्या है?
उत्तर:
बालकों की शिक्षा के दृष्टिकोण से राज्य का मुख्यतम शैक्षिक कार्य है-शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण तथा उसे लागू करना।
प्रश्न 4.
राज्य शिक्षा का औपचारिक/अनौपचारिक अभिकरण है।
उत्तर:
राज्य शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है।
प्रश्न 5.
आपके दृष्टिकोण से शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता तथा एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है।
प्रश्न 6.
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन कर सकता है?
उत्तर:
अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था केवल राज्य ही कर सकता है।
प्रश्न 7.
राज्य शिक्षा के किस अभिकरण का उदाहरण है ?
उत्तर:
औपचारिक अभिकरण।
प्रश्न 8.
निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य
- एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वाले सत्ता सम्पन्न राजनीतिक संगठन को राज्य कहते हैं।
- राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया जा सकता।
- हमारे देश में शिक्षा की नीति का निर्धारण राज्य द्वारा ही किया जाता है।
- शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने का कार्य केवल विभिन्न धार्मिक संस्थाएँ ही कर सकती हैं।
- औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का महत्त्व अधिक है, जब कि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में समाज का महत्त्व अधिक है।
उत्तर:
- सत्य,
- असत्य,
- सत्य,
- असत्य,
- सत्य।
बहुविकल्पीय प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए
प्रश्न 1.
लॉक, मिल तथा बेन्थम आदि व्यक्तिवादी विचारकों की मान्यता है–
(क) शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए।
(ख) शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण एक बुराई है।
(ग) केवल प्राथमिक शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए।
(घ) केवल विज्ञान की शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए।
प्रश्न 2.
सार्वजनिक शिक्षा, जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, एक ऐसा शक्तिशाली यन्त्र
है जो राज्य दूसरों को हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।” यह कथन किसका है।
(क) बेन्थम का
(ख) पिंकविच का
(ग) लॉक का
(घ) प्लेटो का
प्रश्न 3.
हमारे देश में शैक्षिक नीति का निर्धारण किया जाता है
(क) शिक्षकों के द्वारा
(ख) धर्माचार्यों के द्वारा
(ग) राज्य के द्वारा।
(घ) प्रधानमन्त्री के द्वारा
प्रश्न 4.
राज्य का प्रमुख शैक्षिक दायित्व क्या है?
(क) सुरक्षा का प्रबन्ध करना
(ख) अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना
(ग) धर्म का प्रचार करना
(घ) जनशिक्षा का प्रबन्ध करना।
प्रश्न 5.
देश में शिक्षा को एकरूपता प्रदान कर सकता है
(क) समाज
(ख) धर्म
(ग) राज्य
(घ) कोई नहीं
उत्तर:
1. (ख) शिक्षा पर राज्य को नियन्त्रण एक बुराई है,
2. (ख) पिंकविच का,
3. (ग) राज्य के द्वारा,
4. (घ) जनशिक्षा का प्रबन्ध करना,
5. (ग) राज्य।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 10 State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Pedagogy Chapter 10 State: As an Informal Agency of Education (राज्य: शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.