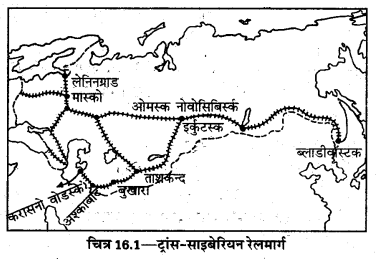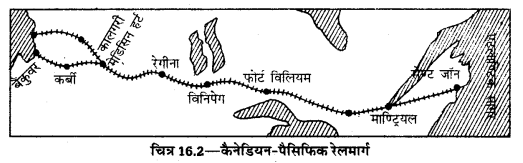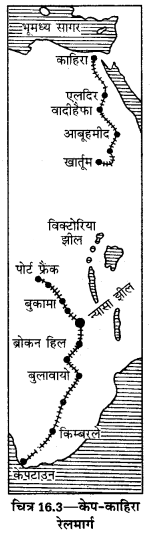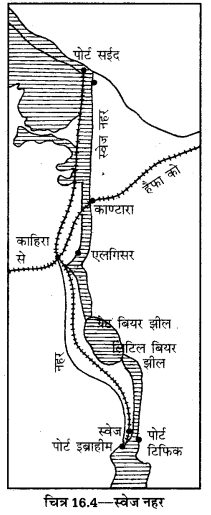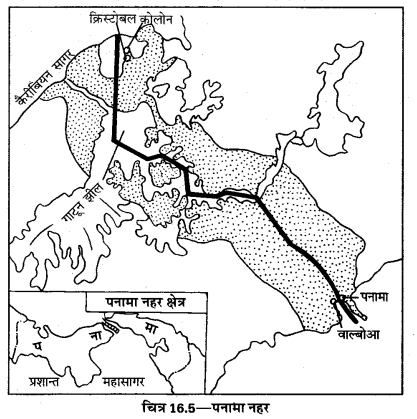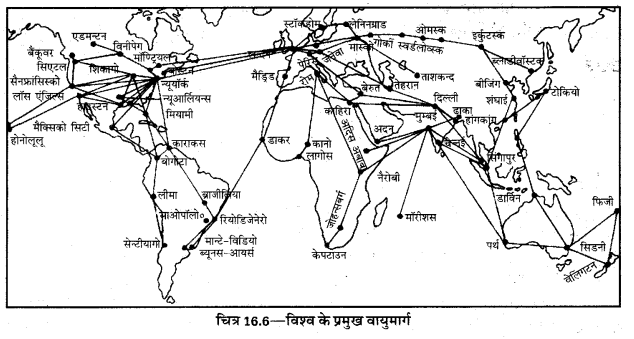UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध are part of UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi . Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध.
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 11 |
| Subject | Sahityik Hindi |
| Chapter | Chapter 3 |
| Chapter Name | राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध
राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध
स्वदेश-प्रेम
सम्बद्ध शीर्षक
- जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
- राष्ट्रधर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
- राष्ट्र के गौरव की सुरक्षा और हमारा कर्तव्य
प्रमुख विचार – बिन्दु
- प्रस्तावना,
- देश प्रेम की स्वाभाविकता,
- देश-प्रेम का अर्थ
- देश-प्रेम का क्षेत्र,
- देश के प्रति कर्तव्य,
- भारतीयों का देश-प्रेम,
- देशभक्तों की कामना
- उपसंहार।
प्रस्तावना – ईश्वर द्वारा बनायी गयी सर्वाधिक अद्भुत रचना है ‘जननी’, जो नि:स्वार्थ प्रेम की प्रतीक है, प्रेम का ही पर्याय है, स्नेह की मधुर बयार है, सुरक्षा का अटूट कवच है, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रक्षिका है, जिसका नाम प्रत्येक शीश को नमन के लिए झुक जाने को प्रेरित कर देता है। यही बात जन्मभूमि के विषय में भी सत्य है। इन दोनों का दुलार जिसने पा लिया उसे स्वर्ग का पूरा-पूरा अनुभव धरा पर ही हो गया। इसीलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। यही कारण है कि स्वदेश से दूर जाकर मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी एक प्रकार की उदासी और रुग्णता का अनुभव करने लगते हैं।
देश-प्रेम की स्वाभाविकता – प्रत्येक देशवासी को अपने देश से अनुपम प्रेम होता है। अपना देश चाहे बर्फ से ढका हुआ हो, चाहे गर्म रेत से भरा हो, चाहे ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से घिरा हो, वह सबके लिए प्रिय होता है। इस सम्बन्ध में कविवर रामनरेश त्रिपाठी की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं
विषुवत् रेखा का वासी जो, जीता है नित हाँफ-हाँफ कर।
रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ॥
ध्रुववासी जो हिम में तम में, जी लेता है काँप-काँप कर।
वह भी अपनी मातृभूमि पर, कर देता है प्राण निछावर ॥
प्रात:काल के समय पक्षी भोजन-पानी के लिए कलरव करते हुए दूर स्थानों के लिए चले जाते हैं परन्तु सायंकाल होते ही एक विशेष उमंग और उत्साह के साथ अपने-अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। पशु-पक्षियों में उसके लिए इतना मोह और लगाव हो जाता है कि वे उसके लिए मर-मिटने हेतु भी तत्पर रहते हैं
आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात,
तुम क्यों जलते पक्षियो! जब पंख तुम्हारे पास?
फल खाये इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात,
यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ।
पशु-पक्षियों को भी अपने घर से, अपनी मातृभूमि से इतना प्यार है तो भला मानव को अपनी जन्मभूमि से, अपने देश से क्यों प्यार नहीं होगा? वह तो विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि, बुद्धिसम्पन्न एवं सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी है। माता और जन्मभूमि की तुलना में स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। संस्कृत के किसी महान् कवि ने ठीक ही कहा है – जननीजन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।
देश-प्रेम का अर्थ – देश-प्रेम का तात्पर्य है – देश में रहने वाले जड़-चेतन सभी प्राणियों से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों, महलों तथा संस्थाओं से प्रेम, देश के रहन-सहन, रीति-रिवाज, वेश-भूषा से प्रेम, देश के सभी धर्मों, मतों, भूमि, पर्वत, नदी, वन, तृण, लता सभी से प्रेम और अपनत्व रखना व उन सभी के प्रति गर्व की अनुभूति करना। सच्चे देश-प्रेमी के लिए देश का कण-कण पावन और पूज्य होता है।
सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर ।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर ॥
देश-प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित ।
आत्मा के विकास से, जिसमें मानवता होती है विकसित ॥
सच्चा देश-प्रेमी वही होता है, जो देश के लिए नि:स्वार्थ भावना से बड़े-से-बड़ा त्याग कर सकता है। स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है और दूसरों को भी उनके उपयोग के लिए प्रेरित करता है। सच्चा देशभक्त उत्साही, सत्यवादी, महत्त्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। वह देश में छिपे हुए गद्दारों से सावधान रहता है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर देश की रक्षा के लिए शत्रुओं का मुकाबला करता है।
देश-प्रेम का क्षेत्र – देश-प्रेम का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। सैनिक युद्ध-भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर, राज-नेता राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त. कर, समाज-सुधारक समाज का नवनिर्माण करके, धार्मिक नेता मानव-धर्म का उच्च आदर्श प्रस्तुत करके, साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना और जन-जागरण का स्वर फेंककर, कर्मचारी, श्रमिक एवं किसान निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करके, व्यापारी मुनाफाखोरी व तस्करी का त्याग कर अपनी देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। ध्यान रहे, सभी को अपना कार्य करते हुए देशहित को सर्वोपरि समझनी चाहिए।
देश के प्रति कर्त्तव्य – जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत समान जल पीकर, सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान् हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल-कूदकर हमने पुष्ट शरीर प्राप्त किया है, उस देश के प्रति हमारे अनन्त कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्यपालन और त्याग की भावना से श्रद्धा, सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। हमें अपने देश की एक इंच भूमि के लिए तथा उसके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। यह सब करने पर भी जन्मभूमि या अपने देश से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं।
भारतीयों का देश-प्रेम – भारत माँ ने ऐसे असंख्य नर-रत्नों को जन्म दिया है, जिन्होंने असीम त्याग-भावना से प्रेरित होकर हँसते-हँसते मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित कर दिये। कितने ही ऋषि-मुनियों ने अपने तप और त्याग से देश की महिमा को मण्डित किया है तथा अनेकानेक वीरों ने अपने अद्भुत शौर्य से शत्रुओं के दाँत खट्टे किये हैं। वन-वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाना स्वीकार किया, परन्तु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने कभी मस्तक नहीं झुकाया। शिवाजी ने देश और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए गुफाओं में छिपकर शत्रु से टक्कर ली और रानी लक्ष्मीबाई ने महलों के सुखों को त्यागकर शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीरगति प्राप्त की। भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकउल्ला खाँ आदि न जाने कितने देशभक्तों ने विदेशियों की अनेक यातनाएँ सहते हुए, मुख से वन्दे मातरम्’ कहते हुए हँसते-हँसते
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥
भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों को साक्षी है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और मान-मर्यादा के लिए अपने सुखों को त्याग दिया और मन में मर-मिटने का अरमान लेकर शत्रु पर टूट पड़े। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, लाला लाजपतराय आदि अनेक देशभक्तों ने अनेक कष्ट सहकर और प्राणों का बलिदान करके देश की स्वाधीनता की ज्योति को प्रज्वलित किया। इसी स्वदेश प्रेम के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनेकों कष्ट सहे, जेलों में रहे तथा अन्त में अपने प्राण निछावर कर दिये। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभभाई पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू आदि देशरत्नों ने आजीवन देश की सेवा की। श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की एकता और अखण्डता के लिए नृशंस आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बनीं।।
देशभक्तों की कामना – देशभक्तों को सुख-समृद्धि, धन, यश, कंचन और कामिनी की आकांक्षा नहीं होती है। उन्हें तो केवल अपने देश की स्वतन्त्रता, उन्नति और गौरव की कामना होती है। वे देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। मृत्यु के समय भी उनकी इच्छा यही होती है कि वे देश के काम आयें। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में एक पुष्प की भी यही कामना है
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक॥
उपसंहार – खेद का विषय है कि आज हमारे नागरिकों में देश-प्रेम की भावना अत्यन्त दुर्लभ होती जा रही है। नयी पीढ़ी का विदेशों से आयातित वस्तुओं और संस्कृतियों के प्रति अन्धाधुन्ध मोह, स्वदेश के बजाय विदेश में जाकर सेवाएँ अर्पित करने के सजीले सपने वास्तव में चिन्ताजनक हैं। हमारी पुस्तकें भले ही राष्ट्रप्रेम की गाथाएँ पाठ्य-सामग्री में सँजोये रहें, परन्तु वास्तव में नागरिकों के हृदय में गहरा व सच्चा राष्ट्रप्रेम ढूंढ़ने पर भी उपलब्ध नहीं होता। हमारे शिक्षाविदों व बुद्धिजीवियों को इस प्रश्न का समाधान ढूंढ़ना ही होगा कि अब मात्र उपदेश या अतीत के गुणगान से वह प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से सुधारनी होगी।
प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश भारत की देशरूपी बगिया में राज्यरूपी अनेक क्यारियाँ हैं । किसी एक क्यारी की उन्नति एकांगी उन्नति है और सभी क्यारियों की उन्नति देशरूपी उपवन की सर्वांगीण उन्नति है। जिस प्रकार एक माली अपने उपवन की सभी क्यारियों की देखभाल समान भाव से करती है उसी प्रकार हमें भी देश का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य न मानकर समग्रतापूर्ण चिन्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि सबकी उन्नति में एक की उन्नति तो अन्तर्निहित होती ही है। प्रत्येक देशवासी का चिन्तन होना चाहिए कि “यह देश मेरा शरीर है और इसकी क्षति मेरी ही क्षति है।’ जब ऐसे भाव प्रत्येक भारतवासी के होंगे तब कोई अपने निहित स्वार्थों के पीछे रेल, बस अथवा सरकारी सम्पत्तियों की होली नहीं जलाएगा और न ही सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग ही करेगा।
स्वदेश-प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसे संकुचित रूप में ग्रहण न करे व्यापक रूप में ग्रहण करना चाहिए। संकुचित रूप में ग्रहण करने से विश्व शान्ति को खतरा हो सकता है। हमें स्वदेश-प्रेम की भावना के साथ-साथ समग्र मानवता के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए।
हमारे राष्ट्रीय पर्व
सम्बद्ध शीर्षक
- भारत के राष्ट्रीय त्योहार
प्रमुख विचार-बिन्दु
- प्रस्तावना,
- गणतन्त्र दिवस,
- स्वतन्त्रता दिवस,
- गांधी जय
- राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य पर्व,
- उपसंहार।
प्रस्तावना – भारतवर्ष को यदि विविध प्रकार के त्योहारों का देश कह दिया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। इस धरा-धाम पर इतनी जातियाँ, धर्म और सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं कि उनके सभी त्योहारों को यदि मनाना शुरू कर दिया जाए तो शायद एक-एक दिन में दो-दो त्योहार मना कर भी वर्ष भर में उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पर्वो का मानव-जीवन व राष्ट्र के जीवन में विशेष महत्त्व होता है। इनसे नयी प्रेरणा मिलती है, जीवन की नीरसता दूर होती है तथा रोचकता और आनन्द में वृद्धि होती है। पर्व या त्योहार कई तरह के होते हैं; जैसे-धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, ऋतु सम्बन्धी और राष्ट्रीय। जिन पर्वो का सम्बन्ध किसी व्यक्ति, जाति या धर्म के मानने वालों से न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र से होता है तथा जो पूरे देश में सभी नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाये जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस एव गांधी जयन्ती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ये राष्ट्रीय पर्व समस्त भारतीय जन-मानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ये उन अमर शहीदों व देशभक्तों का स्मरण कराते हैं, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए जीवन-पर्यन्त संघर्ष किया और राष्ट्र की स्वतन्त्रता, गौरव व इसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अपने प्राणों को भी सहर्ष न्योछावर कर दिया।
गणतन्त्र दिवस – गणतन्त्र दिवस हमारा एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को देशवासियों द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन सन् 1950 ई० में हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हमारा राष्ट्र पूर्ण स्वायत्त गणतन्त्र राज्य बना अर्थात् भारत को पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया। यही दिन हमें 26 जनवरी, 1930 का भी स्मरण कराता है, जब पं० जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था।
गणतन्त्र दिवस का त्योहार बड़ी धूमधाम से यों तो देश के प्रत्येक भाग में मनाया जाता है, पर इसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में ही किया जाता है। इस दिन सबसे पहले देश के प्रधानमन्त्री इण्डिया गेट पर शहीद जवानों की याद में प्रज्वलित की गयी जवान ज्योति पर सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से सलामी देते हैं। उसके बाद प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति महोदय की अगवानी करते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित विजय चौक में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही मुख्य पर्व मनाया जाना आरम्भ होता है। इस दिन विजय चौक से प्रारम्भ होकर लाल किले तक जाने वाली परेड समारोह का प्रमुख आकर्षण होती है। क्रम से तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु), सीमा सुरक्षा बल, अन्य सभी प्रकार के बलों, पुलिस आदि की टुकड़ियाँ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। एन० सी० सी०, एन० एस० एस० तथा स्काउट, स्कूलों के बच्चे सलामी के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए गुजरते हैं। इसके उपरान्त सभी प्रदेशों की झाँकियाँ आदि प्रस्तुत की जाती हैं तथा शस्त्रास्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी जाती है। परेड और झाँकियों आदि पर हेलीकॉप्टरों-हवाई जहाजों से पुष्प वर्षा की जाती है। यह परेड राष्ट्र की वैज्ञानिक, कला व संस्कृति के उत्थान को दर्शाती है। रात को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य राष्ट्रीय महत्त्व के स्थलों पर रोशनी की जाती है, आतिशबाजी होती है और इस प्रकार धूम-धाम से यह राष्ट्रीय त्योहार सम्पन्न होता है।
स्वतन्त्रता दिवस – पन्द्रह अगस्त के दिन मनाया जाने वाला स्वतन्त्रता दिवस का त्योहार भारत का दूसरा मुख्य राष्ट्रीय त्योहार माना गया है। इसके आकर्षण और मनाने का मुख्य केन्द्र दिल्ली स्थित लाल किला है। यों तो समस्त नगर और सम्पूर्ण देश में भी अपने-अपने ढंग से इसे मनाने की परम्परा है। स्वतन्त्रता दिवस प्रत्येक वर्ष अगस्त मास की पन्द्रहवीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन लगभग दो सौ वर्षों के अंग्रेजी दासत्व के पश्चात् हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था। इसी दिन ऐतिहासिक लाल किले पर हमारा तिरंगा झण्डा फहराया गया था। यह स्वतन्त्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भगीरथ प्रयासों व अनेक महान् नेताओं तथा देशभक्तों के बलिदान की गाथा है। यह स्वतन्त्रता इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसे बन्दूकों, तोपों जैसे अस्त्र-शस्त्रों से नहीं वरन् सत्य, अहिंसा जैसे शस्त्रास्त्रों से प्राप्त किया गया। इस दिन सम्पूर्ण राष्ट्र देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए देश की स्वतन्त्रता को बनाये रखने की शपथ लेता है। इस दिवस की पूर्व सन्ध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना सन्देश प्रसारित करते हैं। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले प्रधानमन्त्री सेना की तीनों टुकड़ियों, अन्य सुरक्षा बलों, स्काउटों आदि का निरीक्षण कर सलामी लेते हैं। फिर लाल किले के मुख्य द्वार पर पहुँचकर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर उसे सलामी देते हैं तथा राष्ट्र को सम्बोधित करते हैं। इस सम्बोधन में पिछले वर्ष सरकार द्वारा किये गये कार्यों का लेखा-जोखा, अनेक नवीन योजनाओं तथा देश-विदेश से सम्बन्ध रखने वाली नीतियों के बारे में उद्घोषणा की जाती है। अन्त में राष्ट्रीय गान के साथ यह मुख्य समारोह समाप्त हो जाता है। रात्रि में दीपों की जगमगाहट से विशेषकर संसद भवन व राष्ट्रपति भवन की सजावट देखते ही बनती है।
गांधी जयन्ती – गांधी जयन्ती भी हमारी एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रति वर्ष गांधी जी के जन्म-दिवस 2 अक्टूबर की शुभ स्मृति में देश भर में मनाया जाता है। स्वाधीनता आन्दोलन में गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से देश का नेतृत्व किया और देश को स्वतन्त्र कराने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन से शक्तिशाली अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। गांधी जी ने राष्ट्र एवं दीन-हीनों की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। प्रति वर्ष सम्पूर्ण देश उनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के लिए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बताये गये रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस दिन सम्पूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की सभाओं, गोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गांधी जी की समाधि राजघाट पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री व अन्य विशिष्ट लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी अमर रहें” के नारों से सम्पूर्ण वातावरण गूंज उठता है।
राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य पर्व – इन तीन मुख्य पर्वो के अतिरिक्त अन्य कई पर्व भी यहाँ मनाये जाते हैं. और उनका भी राष्ट्रीय महत्त्व स्वीकारा जाता है। ईद, होली, वसन्त पंचमी, बुद्ध पंचमी, वाल्मीकि प्राकट्योत्सव, विजयादशमी, दीपावली आदि इसी प्रकार के पर्व माने जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता किसी-न-किसी रूप में इन सभी त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी मुख्य महत्त्व उपर्युक्त तीन पर्वो का ही है।
उपसंहार – त्योहार तीन हों या अधिक, सभी का महत्त्व मानवीय एवं राष्ट्रीय अस्मिता को उजागर करना ही होता है। मानव-जीवन में जो एक आनन्दप्रियता, उत्सवप्रियता की भावना और वृत्ति छिपी रहती है, उनका भी इस प्रकार से प्रकटीकरण और स्थापन हो जाया करता है। इस प्रकार के त्योहार सभी देशवासी मिलकर मनाया करते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता और ऊर्जा को भी बल मिलता है जो इनका वास्तविक उद्देश्य एवं प्रयोजन होता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा-स्रोत हैं। ये पर्व सभी भारतीयों के मन में हर्ष, उल्लास और नवीन राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं। साथ ही देशवासियों को यह संकल्प लेने हेतु भी प्रेरित करते हैं कि वे अमर शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे तथा अपने देश की रक्षा, गौरव व इसके उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे।
राष्ट्रीय एकता
सम्बद्ध शीर्षक
- राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक उपाय
- राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता
- राष्ट्रीय एकीकरण और उसके मार्ग की बाधाएँ
- राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्त्व
- राष्ट्रीय अखण्डता – आज की माँग
- भारत की राष्ट्रीय एकता
प्रमुख विचार-बिन्दु
- प्रस्तावना : राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय,
- भारत में अनेकता के विविध रूप,
- राष्ट्रीय एकता का आधार,
- राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता,
- राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाए
(क) साम्प्रदायिकता;
(ख) क्षेत्रीयता अथवा प्रान्तीयता;
(ग) भाषावाद;
(घ) जातिवाद;
(ङ) संकीर्ण मनोवृत्तिा - राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के उपाय
(क) सर्वधर्म समभाव;
(ख) समष्टि हित की भावना;
(ग) एकता का विश्वास;
(घ) शिक्षा का प्रसार;
(ङ) राजनीतिक छल-छयों का अन्त, - उपसंहार ।
प्रस्तावना : राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय – एकता एक भावात्मक शब्द है, जिसका अर्थ है-‘एक होने का भाव’। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय है-देश का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से एक होना। भारत में इन दृष्टिकोणों से अनेकता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु बाह्य रूप से दिखलाई देने वाली इस अनेकता के मूल में वैचारिक एकता निहित है। अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता उसके राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक होती है और जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान नहीं होता, वह मनुष्य नहीं
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं नरपशु है निरा, और मृतक समान है।
भारत में अनेकता के विविध रूप – भारत एक विशाल देश है। उसमें अनेकता होनी स्वाभाविक ही है। धर्म के क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि विविध धर्मावलम्बी यहाँ निवास करते हैं। इतना ही नहीं, एक-एक धर्म में भी कई अवान्तर भेद हैं; जैसे-हिन्दू धर्म के अन्तर्गत वैष्णव, शैव, शाक्त आदि। वैष्णवों में भी रामपूजक और कृष्णपूजक हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी अनेकानेक अवान्तर भेद हैं।
सामाजिक दृष्टि से विभिन्न जातियाँ, उपजातियाँ, गोत्र, प्रवर आदि विविधता के सूचक हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, पूजा-पाठ आदि की भिन्नता ‘अनेकता’ की द्योतक है। राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद आदि अनेक वाद राजनीतिक विचार-भिन्नता का संकेत करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भारत की प्राचीन और नवीन भाषाओं में रचित साहित्य की भिन्न-भिन्न शैलियाँ विविधता की सूचक हैं। आर्थिक दृष्टि से पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराएँ भिन्नता दर्शाती हैं। इसी प्रकार भारत की प्राकृतिक शोभा, भौगोलिक स्थिति, ऋतु-परिवर्तन आदि में भी पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इतनी विविधताओं के होते हुए भी भारत अत्यन्त प्राचीन काल से एकता के सूत्र में बँधा रहा है।
राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सार्वभौमिक सत्ता बनाये रखने के लिए राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना परमावश्यक है। यही वह भावना है, जिसके कारण राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के सम्मान, गौरव और हितों का चिन्तन करते हैं।
राष्ट्रीय एकता का आधार – हमारे देश की एकता के आधार दर्शन (Philosophy) और साहित्य (Literature) हैं। ये सभी प्रकार की भिन्नताओं और असमानताओं को समाप्त करने वाले हैं। भारतीय दर्शन सर्व-समन्वय की भावना का पोषक है। यह किसी एक भाषा में नहीं लिखा गया है, अपितु यह देश की विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। इसी प्रकार हमारे देश का साहित्य भी विभिन्न क्षेत्र के निवासियों द्वारा लिखे जाने के बावजूद क्षेत्रवादिता या प्रान्तीयता के भावों को उत्पन्न नहीं करता, वरन् सबके लिए भाई-चारे, मेल-मिलाप और सद्भाव का सन्देश देता हुआ देशभक्ति के भावों को जगाता है।
राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता – राष्ट्र की आन्तरिक शान्ति, सुव्यवस्था और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है। भारत के सन्तों ने तो प्रारम्भ से ही मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई अन्तर नहीं माना। वह तो सम्पूर्ण मनुष्य जाति को एक सूत्र में बाँधने के पक्षधर रहे हैं। नानक का कथन है
अव्वले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बन्दै।
एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मन्दे॥
यदि हम भारतवासी अपने में निहित अनेक विभिन्नताओं के कारण छिन्न-भिन्न हो गये तो हमारी फूट का लाभ उठाकर अन्य देश हमारी स्वतन्त्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही विचार राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने व्यक्त किया था-‘जब-जब भी हम असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी।” अत: देश की स्वतन्त्रता की रक्षा और राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता का होना परम आवश्यक है।
राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएँ – मध्यकाल में विदेशी शासकों का शासन हो जाने पर भारत की इस अन्तर्निहित एकता को आघात पहुँचा था, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अनेक समाज-सुधारकों और दूरदर्शी राजपुरुषों के सद्प्रयत्नों से यह आन्तरिक एकता मजबूत हुई थी, किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अनेक तत्त्व इस आन्तरिक एकता को खण्डित करने में सक्रिय रहे हैं, जो निम्नवत् हैं
(क) साम्प्रदायिकता – साम्प्रदायिकता धर्म का संकुचित दृष्टिकोण है। संसार के विविध धर्मों में जितनी बातें बतायी गयी हैं, उनमें से अधिकांश बातें समान हैं; जैसे–प्रेम, सेवा, परोपकार, सच्चाई, समता, नैतिकता, अहिंसा, पवित्रता आदि। सच्चा धर्म कभी भी दूसरे से घृणा करना नहीं सिखाता। वह तो सभी से प्रेम करना, सभी की सहायता करना, सभी को समान समझना सिखाता है। जहाँ भी विरोध और घृणा है, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। जाति-पाँति के नाम पर लड़ने वालों पर इकबाल कहते हैं-मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
(ख) क्षेत्रीयता अथवा प्रान्तीयता – अंग्रेज शासकों ने न केवल धर्म, वरन् प्रान्तीयता की अलगाववादी भावना को भी भड़काया है। इसीलिए जब-तब राष्ट्रीय भावना के स्थान पर प्रान्तीय अलगाववादी भावना बलवती होने लगती है और हमें पृथक् अस्तित्व (राष्ट्र) और पृथक् क्षेत्रीय शासन स्थापित करने की माँगें सुनाई पड़ती हैं। एक ओर कुछ तत्त्व खालिस्तान की माँग करते हैं तो कुछ तेलुगूदेशम् और ब्रज प्रदेश के नाम पर मिथिला राज्य चाहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीयता अथवा प्रान्तीयता की भावना भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ी बाधी बन गयी है।
(ग) भाषावाद – भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। प्रत्येक भाषा-भाषी अपनी मातृभाषा को दूसरों से बढ़कर मानता है। फलत: विद्वेष और घृणा का प्रचार होता है और अन्ततः राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत को एक संघ के रूप में गठित किया गया और प्रशासनिक सुविधा के लिए चौदह प्रान्तों में विभाजित किया गया, किन्तु धीरे-धीरे भाषावाद के आधार पर प्रान्तों की माँग बलवती होती चली गयी, जिससे भारत के प्रान्तों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तदुपरान्त कुछ समय तो शान्ति रही, लेकिन शीघ्र ही अन्य अनेक विभाषी बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने अपनी-अपनी विभाषा या बोली के आधार पर अनेक आन्दोलन किये, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को धक्का पहुंचा।
(घ) जातिवाद – मध्यकाल में भारत के जातिवादी स्वरूप में जो कट्टरता आयी थी, उसने अन्य जातियों के प्रति घृणां और विद्वेष का भाव विकसित कर दिया था। पुराकाल की कर्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था ने जन्म पर आधारित कट्टर जाति-प्रथा का रूप ले लिया और प्रत्येक जाति अपने को दूसरी से ऊँची मानने लगी। इस तरह जातिवाद ने भी भारत की एकता को बुरी तरह प्रभावित किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हरिजनों के लिए आरक्षण की राजकीय नीति का आर्थिक दृष्टि से दुर्बल सवर्ण जातियों ने कड़ा विरोध किया। विगत वर्षों में इस विवाद पर लोगों ने तोड़-फोड़, आगजनी और आत्मदाह जैसे कदम उठाकर देश की राष्ट्रीय एकता को झकझोर दिया। इस प्रकार जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आज एक बड़ी बाधा बन गया है।
(ङ) संकीर्ण मनोवृत्ति – जाति, धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर जब लोगों की विचारधारा संकीर्ण हो जाती है, तब राष्ट्रीयता की भावना मन्द पड़ जाती है। लोग सम्पूर्ण राष्ट्र का हित न देखकर केवल अपने जाति, धर्म, सम्प्रदाये अथवा वर्ग के स्वार्थ को देखने लगते हैं।
राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के उपाय – वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत हैं
(क) सर्वधर्म समभाव – विभिन्न धर्मों में जितनी भी अच्छी बातें हैं, यदि उनकी तुलना अन्य धर्मों की बातों से की जाये तो उनमें एक अद्भुत समानता दिखाई देगी; अतः हमें सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर किसी को ऊँचा या नीचा समझना नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक पाप है। धार्मिक सहिष्णुता बनाये रखने के लिए गहरे विवेक की आवश्यकता है। सागर के समान उदार वृत्ति रखने वाले इनसे प्रभावित नहीं होते।
(ख) समष्टि-हित की भावना – यदि हम अपनी स्वार्थ-भावना को त्यागकर समष्टि-हित का भाव विकसित कर लें तो धर्म, क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर न सोचकर समूचे राष्ट्र के नाम पर सोचेंगे और इस प्रकार अलगाववादी भावना के स्थान पर राष्ट्रीय भावना का विकास होगा, जिससे अनेकता रहते हुए भी एकता की भावना सुदृढ़ होगी।
(ग) एकता का विश्वास – भारत में जो दृश्यमान् अनेकता है, उसके अन्दर एकता का भी निवास है—इस बात का प्रचार ढंग से किया जाये, जिससे कि सभी नागरिकों को अन्तर्निहित एकता का विश्वास हो सके। वे पारस्परिक प्रेम और सद्भाव द्वारा एक-दूसरे में अपने प्रति विश्वास जगा सकें।
(घ) शिक्षा का प्रसार – छोटी-छोटी व्यक्तिगत द्वेष की भावनाएँ राष्ट्र को कमजोर बनाती हैं। शिक्षा का सच्चा अर्थ एक व्यापक अन्तर्दृष्टि व विवेक है। इसलिए शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी की संकुचित भावनाएँ शिथिल हों। विद्यार्थियों को मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के साथ एक अन्य प्रादेशिक भाषा का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे भाषायी स्तर पर ऐक्य स्थापित होने से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी।
(ङ) राजनीतिक छलछद्मों का अन्त – विदेशी शासनकाल में अंग्रेजों ने भेदभाव फैलाया था, किन्तु अब स्वार्थी राजनेता ऐसे छलछद्म फैलाते हैं कि भारत में एकता के स्थान पर विभेद ही अधिक पनपता है। ये राजनेता साम्प्रदायिक अथवा जातीय विद्वेष, घृणा और हिंसा भड़काते हैं और सम्प्रदाय विशेष को मसीहा बनकर अपना स्वार्थ-सिद्ध करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक छलछद्मों का अन्त राजनीतिक वातावरण के स्वच्छ होने से भी एकता का भाव सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। उपर्युक्त उपायों से भारत की अन्तर्निहित एकता का सभी को ज्ञान हो सकेगा और सभी उसको खण्डित करने के प्रयासों को विफल करने में अपना योगदान कर सकेंगे। इस दिशा में धार्मिक महापुरुषों, समाज-सुधारकों, बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और महिलाओं को विशेष रूप से सक्रिय होना चाहिए तथा मिल-जुलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर सबल राष्ट्र के घटक स्वयं भी अधिक पुष्ट होंगे।
उपसंहार – राष्ट्रीय एकता की भावना एक श्रेष्ठ भावना है और इस भावना को उत्पन्न करने के लिए हमें स्वयं को सबसे पहले मनुष्य समझना होगा, क्योंकि मनुष्य एवं मनुष्य में असमानता की भावना समस्त विद्वेष एवं विवाद का कारण है। इसीलिए जब तक हममें मानवीयता की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यह भाव उपदेशों, भाषणों और राष्ट्रीय गीत के माध्यम से सम्भव नहीं।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Sahityik Hindi राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.