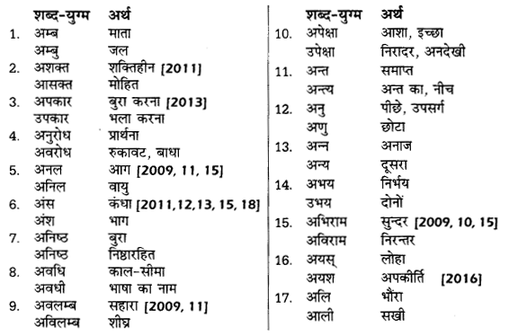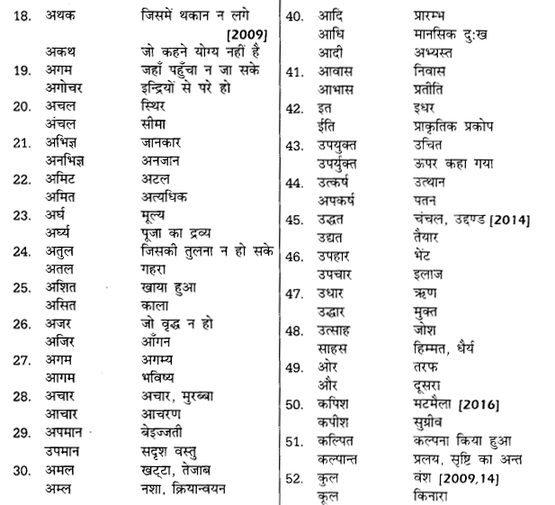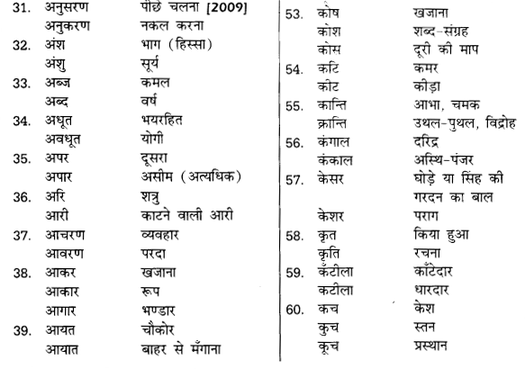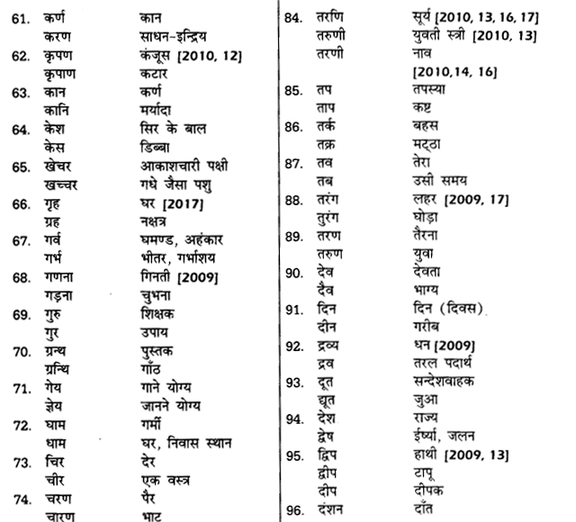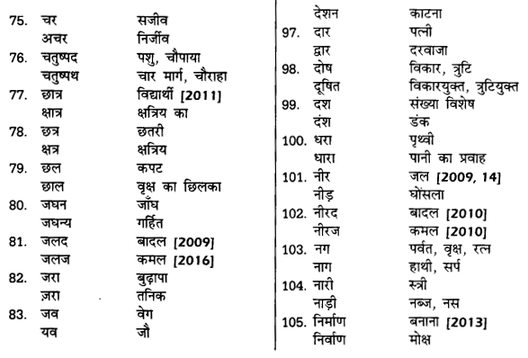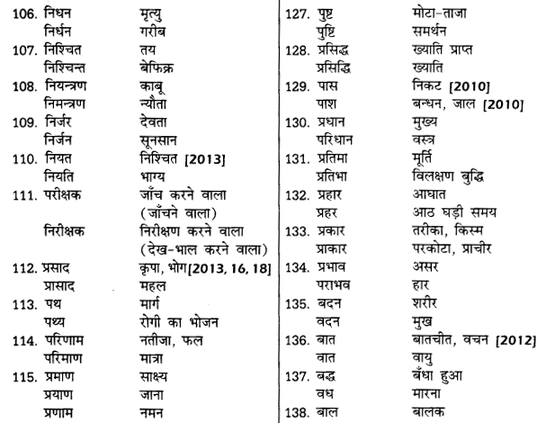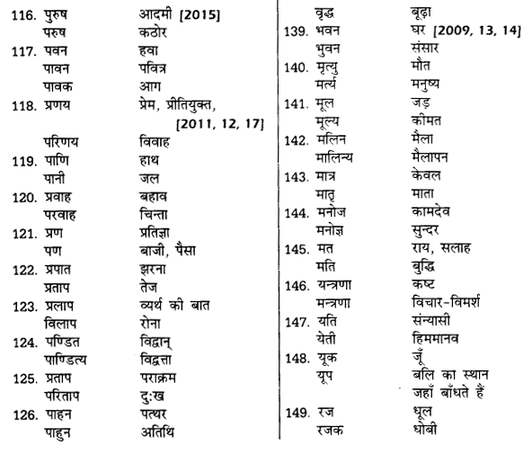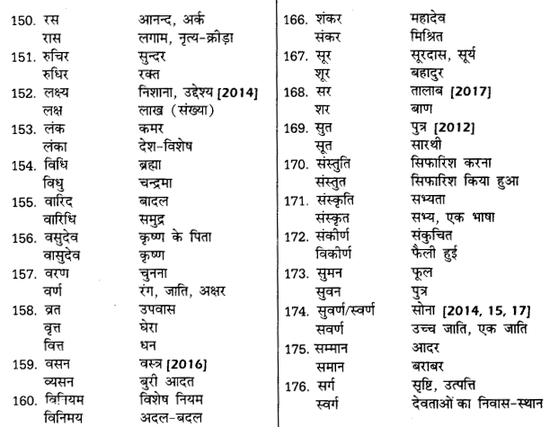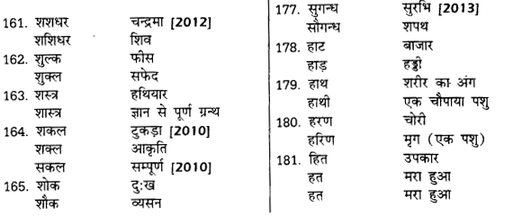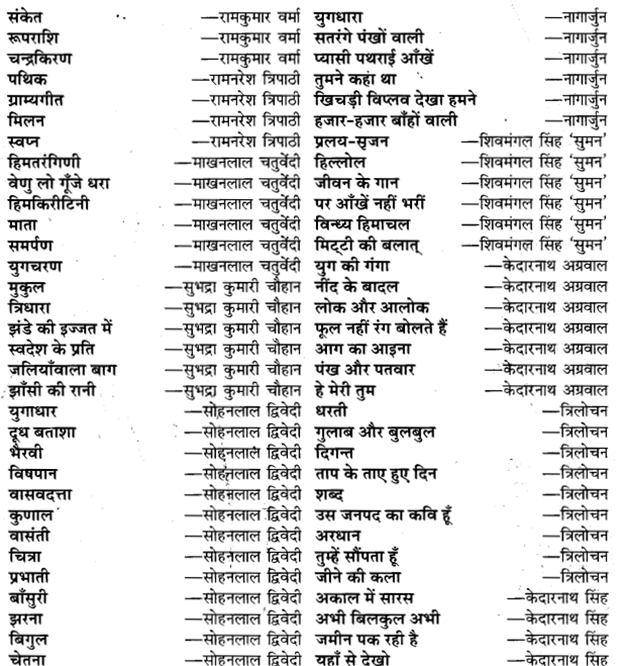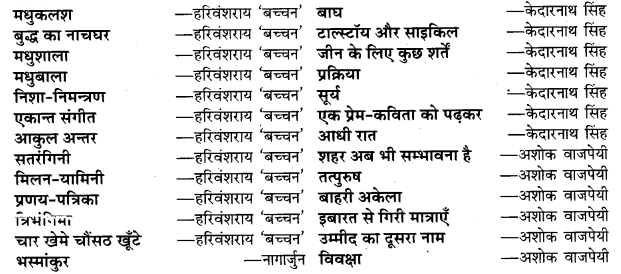UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 9 Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ) are part of UP Board Solutions for Class 12 Geography. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 9 Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ).
| Board | UP Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 12 |
| Subject | Geography |
| Chapter | Chapter 9 |
| Chapter Name | Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ) |
| Number of Questions Solved | 14 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 9 Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के कारक बताइए तथा विकास-क्रम के आधार पर नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिएं। नगरीकरण से क्या तात्पर्य है?
या
नगरीकरण की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। [2014, 16]
या
नगरीय अधिवास की मुख्य विशेषताएँ बताइए तथा कार्यों के अनुसार नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए।
या
नगरीय अधिवास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (2015)
नगरीय अधिवास
Urban Settlement
नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा-तकनीकी, संस्कृति एवं मनोरंजन के केन्द्र होते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में कुछ अन्तर होता है- ग्रामीण अधिवास तो प्राथमिक व्यवसायों; जैसे-आखेट, मत्स्य संग्रहण, पशुचारण, कृषि आदि कार्य करने वाले लोगों की बस्तियाँ होती हैं, जबकि नगरीय अधिवास अकृषित कार्यों; जैसे- निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, उच्च सेवाओं, प्रशासनिक आदि कार्य करने वाले लोगों की बस्तियाँ होती हैं। इन नगरीय अधिवासों द्वारा इन कार्यों में से एक अथवा दो व्यवसाय या सभी कार्य भी किये जा सकते हैं।
नगरीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएँ
Meaning and Definitions of Urbanization
नगरीकरण वर्तमान युग की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यद्यपि आज से हजारों वर्ष पूर्व भी पृथ्वी पर नगर थे परन्तु उस समय नगरीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त मन्द थी। वस्तुतः नगरीकरण का आशय व्यक्तियों द्वारा शहरी संस्कृति को स्वीकार करना है। नगरीकरण की निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा इस तथ्य को ठीक प्रकार समझा जा सकता है –
- एण्डरसन के अनुसार, “गाँव से नगर की ओर जनसंख्या के गतिशील होने, साथ ही ग्रामीण जीवन के नगरीय जीवन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है।”
- ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, “गाँवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानान्तरण ही नगरीकरण कहलाता है।”
नगरीय अधिवास की विशेषताएँ
Characteristics of Urban Settlement
- नगर मिश्रित मकानों अथवा इमारतों का एक समूह होता है। इसमें निम्न, मध्यम एवं उच्च आय वर्गों के निवासस्थान, वाणिज्य क्षेत्र, कारखाने, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन, व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य विकसित होते हैं। प्रशासनिक इकाइयाँ भी नगरीय व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं।
- नगरों में व्यावसायिक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। इनके अधिकांश निवासी निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार-वाणिज्य, उच्च सेवाओं तथा प्रशासनिक आदि कार्यों में लगे होते हैं।
- नगरों में संगठित मकान अधिक पाये जाते हैं। यहाँ अनेक मंजिल वाले भवन बनाये जाते हैं। मकानों में सोने के कमरे, स्नानगृह, शौचालय तथा रसोईघर आदि सुविधाओं की पृथक् व्यवस्था होती है।
- नगरों में पक्की सड़कें तथा गलियाँ होती हैं। ये परिवहन मार्गों के केन्द्र होते हैं। इनमें गन्दे जल के निकास की व्यवस्था नालियों द्वारा की जाती है।
- नगरों में रोशनी, पेयजल, स्वच्छता एवं शान्ति बनाये रखने की भी व्यवस्था होती है।
- नगरों में व्यावसायिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आदि विभिन्न संस्थान भी होते हैं, जो नगरीय जीवन के आवश्यक एवं गतिशील अंग होते हैं।
- नगरों में परिवहन, संचार एवं दूरसंचार के साधनों की भी समुचित व्यवस्था होती है। यहाँ वनों का कर्णभेदी शोर तथा ग्रामीण प्रदेशों से आने वाले दैनिक व्यक्तियों की भीड़-भाड़ अधिक रहती है।
- अनेक नगर सुनियोजित ढंग से बसाये जाते हैं। इनमें पार्क, जल प्रदाय, धर्मशालाएँ आदि सार्वजनिक स्थान भी समुचित ढंग से बनाये जाते हैं।
- नगरों में सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाओं में विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक विकास केन्द्र, खेल के मैदान, पार्क, क्लब, सिनेमाघर आदि भी पाये जाते हैं।
- नगरीय जीवन प्राकृतिक पर्यावरण से दूर फैशन एवं कृत्रिमता से पूर्ण होते हैं।
नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के कारक
Origin and Factors of Development of Towns
नगर सांस्कृतिक विकास को प्रदर्शित करते हैं और इनका प्रारम्भ कृषि तथा पशुपालन के परिपक्व स्तर पर पहुँचने के कारण आज से पाँच-छ: हजार वर्षों पूर्व हुआ था। नगरों की उत्पत्ति एवं उनका विकास निम्नलिखित कारकों द्वारा हुआ है –
(1) अतिरिक्त उत्पादन (Surplus Production) – प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन के कारण समाज के कुछ लोगों ने प्राथमिक उत्पादन से अवकाश ले लिया। इससे समाज में शैक्षणिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का प्रसार प्रारम्भ हुआ।
(2) प्रथम नगरीय क्रान्ति (First Urban Revolution) – प्राचीन नवपाषाण युग, जिसे नगरीय क्रान्ति युग’ भी कहते हैं, में नयी उत्पादन विधियों, नये विचार, आविष्कार एवं सृजनात्मक कार्य, कला-कौशल, भाषा, साहित्य, सामाजिक-राजनीतिक संगठन, उद्योग आदि नये कार्य प्रकट हुए। इससे नगरों की उत्पत्ति और उनके विकास आरम्भ हुए। पहले केन्द्रीय गाँव नगर बनने लगे।
(3) क्षेत्रीय केन्द्रीयता (Regional Centrality) – नगर, स्थानीय एवं क्षेत्रीय केन्द्रीयता के कारण विकास कार्यों के लिए केन्द्रीय स्थानों के रूप में उभरे।
(4) राजनीतिक कारक (Political Factors) – राजाओं व सम्राटों ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए नगरीय केन्द्रों को अपनी राजधानी बनाया। ये नगर प्रारम्भ से ही राजकीय शक्ति तथा सामाजिक-आर्थिक कार्यों के केन्द्र बन गये थे। इनके कारण कुछ ग्रामीण बस्तियाँ नगरीय केन्द्रों के रूप में उदित हुई हैं।
(5) आर्थिक, औद्योगिक-व्यापारिक कारक (Economic, Industrial, Commercial Factors) – उद्योग-धन्धे, विभिन्न व्यवसाय, बाजार, मण्डी, राजमहल जैसे- राजकीय कार्य या शिक्षण-प्रशिक्षण आदि संस्थाओं के एक केन्द्रीय स्थल पर एकत्रित होने के कारण नगरों की क्षेत्रीयता की शक्ति बढ़ गयी तथा इनके चारों ओर बसे मानव-समूहों पर राजसत्ता का नियन्त्रण अधिक सम्भव हो गया।
(6) धार्मिक-सामाजिक कारक (Religious-Social Factors) – पश्चिमी एशिया की आरम्भिक सभ्यताओं में राजा न केवल राजसत्ता, बल्कि धार्मिक कार्यों का भी प्रमुख होता था और उसकी सत्ता ईश्वर के रूप में मानी जाती थी। इस प्रकार धर्म एवं राजशक्ति, दोनों के एकजुट होने पर व्यापारिक कार्य तथा अन्य कार्य एक स्थान पर एकत्र होते गये तथा नगरों का भी विकास होता गया।
(7) सुरक्षा केन्द्र (Defence Centres) – राजधानी की सुरक्षा के लिए नगर सैनिक केन्द्र तथा आन्तरिक सुरक्षा केन्द्र बन गये। इन्हीं कारणों से प्राचीन तथा मध्ययुगीन नगर परकोटायुक्त तथा किले वाले बनाये जाते थे।
(8) बहुधन्धी विकास-मूलक कारक (Multi-Developmental Factors) – राजधानी, प्रशासन, धर्मसत्ता, व्यापार, उद्योग-धन्धे, सुरक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, संगठन, विकास, कल्याण आदि सभी कार्यों के एकजुट हो जाने से नगर की सत्ता चारों ओर के समीपवर्ती क्षेत्र पर बढ़ती गयी।
(9) सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors) – कला-कौशल, स्थापत्य कला, संगीत, धर्म आदि के ज्ञाताओं का कार्य-क्षेत्र केन्द्रीय स्थानों और राजधानियों में अधिक था। इसी कारण नगर सांस्कृतिक विकास के केन्द्र हो गये।
आधुनिक औद्योगिक विकास – आधुनिक औद्योगिक युग को द्वितीय नगरीय क्रान्ति’ (Second Urban Revolution) कहा जाता है। आधुनिक उद्योग-धन्धे वृहत् पैमाने पर विकसित हुए हैं। इनमें सम्पूर्ण विश्व में आधुनिक परिवहन साधनों द्वारा कच्चे माल की पूर्ति की जाती है तथा उत्पादों की खपत भी विश्व स्तर पर की जाती है। इस प्रकार पूँजी, श्रम, तकनीकी एवं प्रबन्ध कुशलता, ज्ञान-विज्ञान आदि का आदान-प्रदान विश्व स्तर पर हो गया है; अतः सम्पूर्ण विश्व एक इकाई होता जा रहा है। कृषि, उद्योग, व्यापार एवं परिवहन के क्षेत्र में उत्पन्न क्रान्तियों ने एकजुट होकर नगरीय-क्रान्ति को जन्म दिया है। औद्योगीकरण तथा नगर एक-दूसरे के लिए प्रेरक हो गये हैं।
किसी भी स्थल पर उद्योग-धन्धों के स्थापित होने के साथ-साथ नगर बसना आरम्भ हो जाता है। नगर बसने के साथ ही अन्य कार्य; जैसे-व्यापारिक दुकानें, सेवा करने वाली दुकानें, प्रशासनिक इकाइयाँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनेक कार्य आदि समय के साथ-साथ विकसित होते जाते हैं। पुनः जनसंख्या में वृद्धि से नये उद्योग-धन्धे स्थापित होने प्रारम्भ हो जाते हैं। इस आधार पर औद्योगीकरण से नगरीकरण तथा नगरीकरण से औद्योगीकरण का क्रम विकसित होता जाता है। अत: उद्योग-धन्धों के प्रसार से निम्नलिखित प्रकार के नगरों का विकास होता है –
- खनन नगर
- व्यापारिक नगर
- शैक्षणिक नगर
- मनोरंजन एवं स्वास्थ्यवर्द्धक नगर
- पर्वतीय नगर
- बन्दरगाह या पत्तन नगर
- क्रीड़ा नगर तथा
- परिवहन नगर।
नगरों का वर्गीकरण Classification of Towns
विकास-क्रम के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में लुईस ममफोर्ड एवं ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण हैं –
(अ) लुईस ममफोर्ड का वर्गीकरण Louis Mumford’s Classification
अमेरिकी समाजशास्त्री लुईस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की छः अवस्थाएँ. बतायी हैं, जो निम्नलिखित हैं –
- इओपोलिस – ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित सेवा-केन्द्रों, केन्द्रीय बाजारों या कस्बों को प्राथमिक नगर अर्थात् इओपोलिस कहते हैं। यह नगरीय विकास की प्रारम्भिक अवस्था होती है।
- पोलिस – जब ये सेवा-केन्द्र या केन्द्रीय बाजार पूर्ण नगरों के रूप में विकसित होते हैं तो उन्हें पोलिस कहा जाता है। इनमें परिवहन, व्यापार एवं सेवा संस्थानों आदि का विकास परिपूर्ण हो जाता है।
- मेट्रोपोलिस – ये बड़े केन्द्रीय नगर होते हैं। ये राज्यों या देशों की राजधानियाँ, औद्योगिक नगर एवं व्यापारिक केन्द्र आदि महानगरों के रूप में होते हैं। इनमें पार्क, खेल के मैदान, सड़कें, सांस्कृतिक संस्थान आदि विकसित हो जाते हैं। इनमें उच्च सांस्कृतिक भू-दृश्य देखने को मिलता है।
- मेगालोपोलिस – यह नगरीय विकास का चरम बिन्दु होता है। व्यापार एवं उद्योगों के अतिरिक्तं यहाँ विशाल एवं बहुमंजिले भवन, विलास-स्थल, मनोरंजन केन्द्र, साहित्य एवं कला-कौशल के केन्द्र विशिष्ट रूप में विकसित होते हैं। आर्थिक-सामाजिक स्तर पर कुछ विशेष व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाता है, जिससे इनका पतन होना प्रारम्भ हो जाता है।
- टायरेनोपोलिस – अधिक बड़े आकार की बस्ती, एकाधिकारी प्रभुसत्ता, बेरोजगारी, अपराध और दुष्कर्मों की अधिकता से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से ह्रास करने लगती है। इन नगरों के निवासी इन्हें छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर बसने के लिए चले जाते हैं।
- नेक्रोपोलिस – इस अवस्था में नगर का पतन चरम सीमा तक होता है। इसमें अपराध, दरिद्रता एवं अराजकता फैली रहती है। नगर-निवासियों की धार्मिक-सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है।
( ब ) ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण Griffith Taylor’s Classification
ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की सात अवस्थाएँ बतायी हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है –
(1) पूर्व-शैशवावस्था – यह नगरीय विकास की आरम्भिक अवस्था है। एक सड़क या गली के सहारे-सहारे लोग अस्थायी रूप से बस जाते हैं। यहाँ पर सामान्य आवश्यकता की कुछ दुकानें भी विकसित हो जाती हैं।
(2) शैशवावस्था – नगरीय विकास की इस अवस्था में मुख्य सड़क या गली के समानान्तर एवं लम्बवत् सड़कों व गलियों का विकास होता है। इससे सड़क मार्गों का एक जाल-सा बन जाता है। मुख्य सड़क-मार्गों एवं चौराहों पर विभिन्न दुकानें विकसित हो जाती हैं।
(3) बाल्यावस्था – इस अवस्था में नगर का विकास आरम्भ हो जाता है तथा नगर के केन्द्रीय भाग में चौक जैसा केन्द्रीय व्यापारिक गूर्त (C.B.D.) बन जाता है।
(4) किशोरावस्था – इसमें नगर का केन्द्रीय भाग पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। व्यापार के अतिरिक्त विभिन्न कार्य; जैसे-उद्योग, परिवहन, शिक्षण-प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वित्तीय एवं अन्य नगरीय सामाजिक-सांस्कृतिक सेवाएँ विकसित हो जाती हैं। नगर के बाहर की ओर मुख्य सड़क-मार्गों के सहारे-सहारे और अधिक नगरीय विकास होता है। नयी-नयी सड़कें बनने लगती हैं। समीपवर्ती ग्रामीण प्रदेश के लोग रोजगार की खोज में आने लगते हैं। इस प्रकार नगर के प्रत्येक कार्य का विकास अलग-अलग रूप में होने लगता है।
(5) प्रौढावस्था – इस अवस्था में न केवल व्यापार, उद्योग, परिवहन, सेवा-संस्थानों आदि का ही विकास होता है, बल्कि विभिन्न वर्गों की सामाजिक बस्तियों को भी अलगाव हो जाता है। इस प्रकार रिहायशी क्षेत्र उच्च, मध्यम एवं निम्न श्रेणियों में बँट जाते हैं एवं अपने स्तरों के अनुसार ही नागरिक रहना प्रारम्भ कर देते हैं।
(6) उत्तर-प्रौढावस्था – यह नगरीय विकास की चरम अवस्था है। नगरीय क्षेत्र सघन बसाव वाला हो जाता है। नगर के सुचारु रूप से संचालन के लिए परिवहन मार्गों, गन्दी बस्तियों, सेवा संस्थानों आदि का सुधार एवं नियोजन होना आरम्भ होता है।
(7) वृद्धावस्था – यह नगरों के ह्रास की अवस्था है। जब किसी नगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क उससे कुछ दूरी से होकर जाने लगती है या नगर अपने विकास की समस्याओं को सुलझाने में या उनका पुनरुद्धार करने में असमर्थ रहता है तो नगर का विध्वंस होना प्रारम्भ हो जाता है तथा नागरिक अन्यत्र स्थानों पर बसना आरम्भ कर देते हैं। तक्षशिला, नालन्दा, कन्नौज आदि प्राचीन नगर इसके मुख्य उदाहरण हैं।
प्रश्न 2
नगरीय अधिवासों के प्रकार तथा प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए।
उत्तर
नगरीय अधिवासों के प्रकार
Types of Urban Settlements
कुल जनसंख्या को आधार मानकर विश्व-स्तर पर नगरीय अधिवासों को निम्नलिखित ग्यारह भागों में विभाजित किया गया है –
(1) केन्द्रीय पुरवे या सेवा केन्द्र (Central Hamlets or Service Centre) संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में जहाँ एकल ग्रामीण आवासों का विकास हुआ, वहाँ चार-छः व्यापारिक संस्थानों वाले पुरवे विकसित हुए हैं। इन केन्द्रों में एक परचून की दुकान, ब्यूटीशॉप एवं नाई की दुकान, चर्च, स्कूल, छोटा अस्पताल, पोस्ट ऑफिस आदि पाये जाते हैं। यह एक सेवा केन्द्र की भाँति कार्य करता है।
(2) केन्द्रीय या नगरीय गाँव (Central or Urban Village) – ये पुरवे से बड़े सेवा केन्द्र होते हैं। इनमें 10 से 20 दुकानें एवं संस्थान होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 से 250, ब्रिटेन में 500 एवं : भारत में इनकी जनसंख्या 10,000 व्यक्तियों से भी अधिक होती है।
(3) छोटे कस्बे या (ग्राम-नगर ) ग्रागर केन्द्र (Small Towns or Rural-Urban Centres) – गालपिन (1915) ने ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के बीच वाले अधिवासों को ‘ग्रागर केन्द्र’ का नाम दिया है। ये वास्तव में बड़े एवं प्रभावशाली सेवा केन्द्र होते हैं। यहाँ पर बड़े बैंक, स्टोर, कृषि विकास संस्थाएँ, बस अड्डा आदि विभिन्न सुविधाएँ होती हैं। भारत में जिन बस्तियों को अभी तक कस्बे का नामकरण नहीं दिया गया है, वे इसी प्रकार के सेवा केन्द्र हैं। यहाँ इनकी जनसंख्या 1,000 से 30,000 व्यक्तियों के मध्य पायी जाती है।
(4) छोटे नगर (Small Towns) – अधिकांश देशों में इन छोटे नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 व्यक्ति तक मानी जाती है। सामान्यतया 5,000 से कम; 5,000 से 10,000; 10,000 से 20,000 तथा 20,000 से 50,000 तक के मध्य जनसंख्या रखने वाले अधिवासों को छोटा नगर ही माना गया है। भारत में 5,000 जनसंख्या रखने वाली बस्ती को नगरीय बस्ती का नाम दिया गया है।
(5) मध्यम आकार के नगर (Middle Towns) – विश्व के अधिकांश देशों में 20,000 से 50,000 एवं 50,000 से 1,00,000 तक की जनसंख्या रखने वाले अधिवासों को इस श्रेणी में रखा जाता है। भारत में भी द्वितीय श्रेणी के नगरों की जनसंख्या 50,000 से 1,00,000 व्यक्तियों के मध्य मानी गयी है।
(6) बड़े नगर (Large Cities) – एक लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।
(7) महानगर (Metropolis) – अधिकांशत: पाँच लाख से दस लाख जनसंख्या वाले नगरों को महानगर के नाम से पुकारा जाता है।
(8) दसलाखी महानगर (Milion City) – दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या रखने वाले बड़े नगरों को दसलाखी महानगर कहते हैं। ये नगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दूसरे बड़े महानगरों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं; जैसे-भारत में दिल्ली एवं मुम्बई महानगर।
(9) सन्नगर (Conurbation) – जब एक क्रम तथा एक सूत्र में अवस्थित एक या अधिक केन्द्रीय नगर अन्य छोटे समीपस्थ नगरों के साथ पारस्परिक रूप से कार्यात्मक एवं संरचनात्मक रूप से सम्बद्ध होते हैं तो ऐसी वृहद् महानगरीय श्रृंखला क्रम को ‘नगर संलयन या सन्नगर’ कहते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली महानगर से सहारनपुर नगर को जाने वाले सड़क-मार्ग पर प्रति 10 से 15 किमी के अन्तराल से छोटे-छोटे कस्बों का विकास हुआ है। दिल्ली, शाहदरा, लोनी व गाजियाबाद सन्नगर के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कानपुर-मगखारा-उन्नाव नगर संलयन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
(10) मेगालोपोलिस (Megalopolis) – सन्नगरों से बड़ा मेगालोपोलिस होता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन से लेकर वाशिंगटन तक 600 किमी से अधिक लम्बाई में बसा क्षेत्र एक वृहद् महानगरीय शृंखला है।।
(11) एकुमेनोपोलिस (Ecumenopolis) – कई सौ किलोमीटर तक फैली मानवीय बस्तियों (नगरों) की श्रृंखलाबद्धता को एकुमेनोपोलिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान से लेकर सम्पूर्ण उत्तर भारत के क्रमबद्ध मानव अधिवास 5,000 वर्ष बाद ऐसे क्रमबद्ध वृहद् नगरीय समाज का रूप धारण कर सकते हैं।
वास्तव में सन्नगर, मेगालोपोलिस एवं एकुमेनोपोलिस श्रेणियाँ नगरीय अधिवासों की क्रमबद्धता पर प्रकाश डालती हैं।
नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप
Pattern of Urban Settlements
नगरीय अधिवासों के मुख्य रूप से निम्नलिखित नौ प्रतिरूप पाये जाते हैं –
(1) चेकरबोर्ड प्रतिरूप (Checker-board Pattern) – इस प्रकार के नगरों में सड़कें एक-दूसरे से समकोण पर मिलती हैं और परस्पर समानान्तर होती हैं। यह प्रतिरूप आयताकार होता है। इसे ‘ग्रिड प्रतिरूप’ भी कहते हैं। वर्तमान परिवहन युग में मोटर मार्गों के लिए यह एक उत्तम प्रणाली है। भारतवर्ष में बंगलुरु, नागपुर, इन्दौर, भोपाल, अमृतसर, जयपुर, चण्डीगढ़ आदि नगरों में यह पद्धति पायी जाती है।
(2) अरीय प्रतिरूप (Radial Pattern) – परिवहन साधनों के केन्द्र पर बसे नगर केन्द्र के चारों ओर निकले मार्गों और सड़कों के किनारे बसते जाते हैं। ऐसे नगर अरीय रूप धारण कर लेते हैं। इसका विकसित रूप मकड़ी के जाल की भाँति लगता है। लन्दन, बर्लिन, पेरिस, दिल्ली आदि नगरों का प्रतिरूप, ऐसा ही है।
(3) तारा प्रतिरूप (Star Pattern) – जब अरीय प्रतिरूप वाले नगर का विकास बाह्य मार्गों पर दूर तकै विस्तृत फैलाव के साथ-साथ होता जाता है, तब नगर का विन्यास तारे जैसा हो जाता है।
(4) वृत्ताकार प्रतिरूप (Circular Pattern) – प्राचीन काल में नगरों का विकास संकेन्द्रीय प्रतिरूप में विकसित होता था। इनके चारों ओर दीवारें, प्राचीरें, गहरी खाइयाँ, किले आदि विकसित होते थे तथा उनका प्रतिरूप वृत्ताकार हो जाया करता था। इनके मध्य में राजमहल या व्यापारिक क्षेत्र होते थे। सड़कें वृत्ताकार होती थीं। आगरा, जयपुर, बीजापुर या पुरानी दिल्ली आदि नगर इसी प्रतिरूप द्वारा निर्मित हुए हैं।
(5) रेखीय प्रतिरूप (Linear Pattern) – कभी-कभी किसी सड़क, रेलमार्ग, नदी या नहर आदि के किनारे-किनारे लगातार नगर का फैलाव होता जाता है, जिसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं।
(6) मिश्रित प्रतिरूप (Mixed Pattern) – विश्व में अधिकांश नगर मिश्रित प्रतिरूपों में विकसित हुए हैं। इनमें कहीं पर वृत्ताकार, कहीं रेखीय, कहीं ग्रिड प्रतिरूप आदि मिश्रित होते हैं।
(7) पंखा प्रतिरूप (Fan Pattern) – जब नगर किसी समुद्री-तट पर या किसी बड़ी नदी के किनारे लम्बे रूप में विकसित हो तो उससे कई सड़कें पीछे की ओर विकसित हो जाती हैं। इन पीछे के मार्गों के सहारे फैली बस्ती पंखे के रूप में विकसित हो जाती है। चेन्नई इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
(8) अनाकार प्रतिरूप (Amorphous Pattern) – कई नगरों का प्रतिरूप आकृतिहीन लगता है। कई छोटे नगरों का विकास इसी प्रकार होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में लार एवं उत्तराखण्ड में रुद्रपुर आदि छोटे नगर इसके उत्तम उदाहरण हैं।
(9) अन्य प्रतिरूप (Other Patterns) – अधिकांश छोटे नगरों की आकृति अंग्रेजी के अक्षर 7 आदि प्रतिरूपों में होती है। झीलों व नदी-मोड़ों पर बसे नगरों का प्रतिरूप अर्द्ध-चन्द्राकार हो जाता है।
प्रश्न 3
नगरों का कार्यों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। नगरों में विभिन्न सुविधाओं एवं समस्याओं का आकलन कीजिए तथा इनका समाधान भी बताइए।
या
नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं के हल के लिए उपायों की विवेचना कीजिए। [2007, 10, 12]
या
कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत कीजिए तथा भारत के सन्दर्भ में नगरीकरण की समस्याओं की विवेचना कीजिए। [2016]
या
नगरीय अधिवास के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। नगरीय अधिवासों के कार्यों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। [2010, 16]
या
टिप्पणी लिखिए-नगरीकरण की समस्याएँ। [2010]
या
नगरीकरण की प्रमुख समस्याओं का विवरण दीजिए तथा उनके समाधान हेतु उपायों को सुझाइए। [2012]
या
कार्यों के आधार पर नगरीय अधिवास को वर्गीकृत कीजिए। [2012]
उत्तर
नगरों का कार्यिक वर्गीकरण Functional Classification of Towns
वर्तमान समय में अधिकांश नगरों में अनेक कार्य किये जाते हैं। इनमें से कुछ किसी एक कार्य में ही विशेषीकृत भी हो गये हैं। इन नगरों में उद्योग, व्यापार, परिवहन, बन्दरगाह, प्रशासन, उत्खनन, सुरक्षा, शिक्षा, धार्मिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि विशिष्ट कार्य भी मिलते हैं, परन्तु नगरों के कार्यों में विशिष्टीकरण के साथ-साथ अन्य कार्य भी मिलते हैं। विशिष्ट कार्य एवं व्यवसाय की प्रमुखता के आधार पर नगरों को अग्रलिखित आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –
(1) प्रशासनिक नगर (Administrative Towns) – देश, राज्य या बड़े प्रदेश की राजधानियों का प्रमुख कार्य प्रशासन होता है। ऐसे नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। इनमें प्रशासनिक कार्यालय व विभिन्न इमारतों आदि की भरमार रहती है। भारत में नई दिल्ली पूर्णतया प्रशासनिक नगर है। इसी प्रकार वाशिंगटन (डी० सी०), इस्लामाबाद, ब्रासीलिया, बर्लिन, कैनबरा, बीजिंग, मास्को आदि प्रशासनिक नगर हैं।
(2) औद्योगिक नगर (Industrial Towns) – जिन नगरों में उद्योग-धन्धों की प्रधानता होती है. उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं। कच्चा माल, ईंधन और ऊर्जा, श्रम, व्यापार, बाजार, यातायात, पूँजी, बैंकिंग, जलापूर्ति, आयात-निर्यात आदि की सुविधाओं के केन्द्रीकरण होने से ऐसे नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो जाती है। ग्लासगो, बर्मिंघम, मानचेस्टर, पिट्सबर्ग, मैंगनीटोगोर्क, कानपुर, मुम्बई, अहमदाबाद आदि औद्योगिक नगर हैं।
(3) व्यापारिक नगर (Commercial Towns) – इन नगरों में व्यापार प्रमुख कार्य होता है। न्यूयॉर्क, लन्दन, हांगकांग, सिंगापुर, कोलकाता आदि व्यापारिक नगर हैं। इस प्रकार के नगर यातायात एवं परिवहन के केन्द्र भी होते हैं।
(4) परिवहन नगर (Transport Towns) – वें नगरे जो परिवहन कार्यों की प्रमुखता रखते हैं, उन्हें परिवहन नगर कहते हैं। शिकागो, पर्थ, वेनिस, मुगलसराय आदि ऐसे ही नगरों के उदाहरण हैं।
(5) खनन नगर (Mining Towns) – खनिज पदार्थ वाले क्षेत्रों में ऐसे नगरों का विकास होता है। झारखण्ड में कोडरमा और गिरिडीह; कर्नाटक में कोलार खनन नगर हैं। इसी प्रकार विश्व के अन्य भागों में जोहांसबर्ग (दक्षिणी अफ्रीका), कालगूर्ती-कुलगार्डी (ऑस्ट्रेलिया), स्क्राण्टन (सं० रा० अ०) तथा सडबरी (कनाडा) प्रमुख खनन केन्द्र हैं। खनिज भण्डार समाप्त हो जाने पर ऐसे नगर उजड़ जाते हैं। इन्हें प्रेत नगर (Ghost Towns) भी कहते हैं।
(6) मण्डी या बाजार नगर (Market Towns) – कृषि या पशुचारण प्रदेशों में विभिन्न वस्तुओं के संग्रहण और वितरण केन्द्रों के रूप में बाजारों या मण्डियों का विकास होता है। ब्रिटेन का नार्विक, उत्तर प्रदेश का हापुड़, बिहार का बिहार-शरीफ, घाना का कुमासी ऐसे ही नगर हैं। ऐसी मण्डियाँ समय के स्मथ-साथ व्यापारिक नगरों का रूप ले लेती हैं।
(7) सुरक्षा केन्द्र (Defence Towns) – सैनिक छावनियाँ, किले वाले अथवा नौ-सेना अथवा वायु सेना मुख्यालय वाले केन्द्र सुरक्षा नगर कहलाते हैं। ये प्रमुख नगरों से अलग क्षेत्र में उदित होते हैं। पाकिस्तान में रावलपिण्डी, भारत में काम्पटी एवं शिलांग ऐसे ही नगर हैं।
(8) सांस्कृतिक-धार्मिक-शैक्षिक नगर (Cultural-Religious-Educational Towns) – इन नगरों में संस्कृति, धर्म एवं शिक्षा का बोलबाला होता है अर्थात् इनमें इन्हीं कार्यों की प्रधानता होती है। वाराणसी इसका सर्वोत्तम नमूना है। इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी की संज्ञा दी जाती है। ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जर्मनी का हाइडेलबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रिंस्टन, स्वीडन का लुण्ड,नीदरलैण्ड का लीडेन विश्व-प्रसिद्ध शैक्षणिक-सांस्कृतिक नगर हैं। इसी प्रकार रोम, येरुसलम, मक्का, हरिद्वार आदि धार्मिक नगर हैं।
नगरों की विशेषताएँ या गुण
Characteristics or Merits of Towns
नगरों में मानवोपयोगी अनेक सुविधाएँ पायी जाती हैं जिनके आकर्षण से समीपवर्ती प्रदेश के लोग यहाँ रहने के लिए प्रवास कर जाते हैं अथवा अपनी सेवाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। ये सुविधाएँ (गुण) निम्नलिखित हैं –
- नगरों में आजीविका के अनेक साधन होते हैं जिससे वहाँ पर रोजगार मिलने में सुविधा रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार होने के कारण बहुत-से लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है जिससे ये लोग रोजगार की तलाश में नगरों को पदार्पण कर जाते हैं।
- नगरों में परिवहन के अनेक साधनों-घोड़ागाड़ी, मोटरगाड़ी, नगर बस-सेवा, टैक्सी, रेलगाड़ी आदि की सुविधा मिलती है।
- नगरों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन, विद्युत तथा जल-आपूर्ति की सुविधाएँ होती हैं।
- नगरों में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण-प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयी-शिक्षा की सुविधाएँ अधिक मिलती हैं।
- सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रबन्ध की व्यवस्था नगरों में उपलब्ध रहती है।
- नगरों में संचार के साधनों; जैसे—डाक, तारघर, टेलीफोन तथा समाचार-पत्रों की सुलभता पायी जाती है।
- नगरीय लोगों के रहन-सहन का स्तर उच्च होता है। अत: इस स्तर को बनाये रखने के लिए एवं अपने कार्यों की देखभाल के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण बहुत-से लोग ग्रामों को छोड़कर नगरों में बस जाते हैं।
- नागरिक प्रशासन नगर में जल, सीवर, विद्युत, सफाई, चिकित्सा आदि अनेक कार्यों का प्रबन्ध करता है। यह व्यवस्था ग्रामों में नहीं पायी जाती है।
- नगरों में विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक स्थान मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ–संगीतालय, सिनेमाघर आदि मनोरंजन के साधनों का आकर्षण बना रहता है।
- ग्रामों में जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने लिए नौकरी की खोज में नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं।
नगरों की समस्याएँ या दोष
Problems or Demerits of Towns
नगरों में सुविधाओं के साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी होती हैं जिनका समाधान खोजना अत्यावश्यक है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं –
- जनसंख्यां में अतिशय वृद्धि के कारण नगरों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है जिससे नगरों में जनसंख्या की सघनता की समस्या हो जाती है। खाली भूमि महँगी हो जाती है। नगर के निवासी छोटे-छोटे मकानों में रहने को विवश हो जाते हैं। यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर प्रात:काल तथा सायंकाल जनसंख्या की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है।
- नगरों में प्राथमिक आवश्यकताओं-दूध, अनाज, साग-सब्जी, फल आदि-की पूर्ति समीपवर्ती देहात क्षेत्रों से की जाती है। कभी-कभी उत्पादन की कमी से या अन्य कमी के कारण इनके मूल्य ऊँचे हो जाते हैं। धनी लोग तो अधिक मूल्य देकर इन वस्तुओं को खरीद लेते हैं, जब कि साधारण आय के लोग देखते ही रह जाते हैं।
- नगरीय क्षेत्रों में खाद्य-पदार्थों; जैसे-आटे, घी, तेल, दूध आदि में मिलावटे बहुत अधिक होती है, जिससे लोगों को भोज्य-पदार्थ भी शुद्ध नहीं मिल पाते।
- नगरीय केन्द्रों के मकानों का किराया बहुत ऊँचा होता है। कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर आदि नगरों में काफी व्यक्ति बिना मकान, रात्रि में नगर की सड़कों की पटरियों पर, पार्क, गलियों या गन्दी बस्तियों में ही सो जाते हैं। इससे वर्ग-संघर्ष की भावना को बल मिलता है।
- भारत के कुछ नगरों में जनसंख्या की सघनता बहुत अधिक है जितनी कि विश्व के वृहत्तम् नगरों में भी नहीं है। मुम्बई महानगर में 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही निवास करते हैं।
- न्यूयॉर्क आदि नगरों में इतनी जनसंख्या की सघनता औसत रूप से 15 या 20 मंजिल के मकानों में रहकर है, परन्तु भारत में उससे अधिक सघनता केवल एक या दो मंजिलों के मकानों में रहते हुए है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरों में लोग बहुत तंग जगह में निवास करते हैं।
- कभी-कभी बड़े नगरों में पेयजल तथा विद्युत-आपूर्ति की कमी से बड़ी असुविधा हो जाती है।
- नगरों के आकार में वृद्धि होने पर उनके प्रबन्ध एवं प्रशासन की समस्या आती है।
- नगरों में समीपवर्ती ग्रामों में जो लोग आकर बसते हैं, वे अधिकतर पुरुष होते हैं। इस कारण नगरों की जनसंख्या में पुरुष-महिला अनुपात का सन्तुलन बिगड़ जाता है।
- बड़े नगरों के लिए पुलिस आदि की व्यवस्था अधिक करनी पड़ती है, जिससे कर आदि अधिक लगते हैं और महँगाई बढ़ जाती है।
- बड़े-बड़े नगर देश की सम्पत्ति होते हैं; अत: युद्ध-काल में बड़े नगरों को बम वर्षा का भय बना रहता है। द्वितीय महायुद्ध में जापान के केवल दो नगरों-हिरोशिमा एवं नागासाकी–पर अणुबम के प्रहार से जापान को हार मान लेनी पड़ी थी। इसीलिए बड़े नगरों को सुरक्षा की भी एक समस्या रहती
- बड़े नगरों में सामाजिक-आर्थिक वर्गों की विषमता की समस्या बहुत गम्भीर हो जाती है। श्रमिक आन्दोलन, हड़ताले आदि बढ़ जाती हैं। धनी एवं निर्धनों में वर्गभेद उत्पन्न हो जाते हैं।
नगरों की समस्याओं का समाधान Remedies of Urban Problems
नगरों के दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नगरों का पुनर्निर्माण किया जाए और मास्टर प्लान योजनाओं द्वारा इन दोषों को दूर किया जाये तथा औद्योगिक क्षेत्रों का भी सुनियोजित विकास किया जाए। योजनाओं द्वारा नगरों के बाह्य विस्तृत भागों में, चौड़ी सड़कों के सहारे-सहारे कम मंजिलों की बस्तियाँ बसाई जानी चाहिए। मिलों एवं कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए मिलों से दूर एवं नगरों के बाह्य भागों में साफ-सुथरे, स्वास्थ्यवर्द्धक मौहल्ले या वार्ड बसाये जाएँ तथा उनके रिहायशी क्षेत्रों से दैनिक काम करने वाले स्थानों तक परिवहन के साधनों-मोटर, बसों या रेलगाड़ियों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। नगर-निर्माण की योजनाएँ बनाने के लिए भूगोलवेत्ताओं का सहयोग अति आवश्यक है। नगर में चौड़ी सड़कें, विद्युत, जल-आपूर्ति, चिकित्सा एवं शिक्षा और रोजगार की योजनाएँ बनाकर उनको तत्परता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
नगरीकरण किसे कहते हैं? [2010, 14, 16]
या
नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। [2008]
उत्तर
नगरीकरण को अंग्रेजी में Urbanization कहा जाता है। इसका अर्थ है-व्यक्ति या जनसंख्या को नगरीय बना देना अर्थात् ऐसी जनसंख्या को, जो ग्रामीण या अर्द्ध-ग्रामीण है, नगरीय जनसंख्या के रूप में परिवर्तित करना नगरीकरण कहलाता है। वास्तव में यदि मनुष्यों का चिन्तन, आचार-विचार तथा सामाजिक मूल्य नगरीय है तो वे ग्रामों में रहते हुए भी नगरीकृत हैं, परन्तु यहाँ पर हमारा उद्देश्य समाज के उस वर्ग से है जो प्रायः अकृषि कार्यों में लगा हुआ है; अतः नगरीकरण . सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसलिए बर्गेल (E. E. Bergel) ने कहा है कि ग्रामों के नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अत: नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो वर्तमान समय की महत्त्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। यह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
प्रश्न 2
नगरीकरण की समस्या के निराकरण के किन्हीं दो उपायों का वर्णन कीजिए।
उत्तर
नगरीय समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित दो उपाय किये जा सकते हैं –
- नगरों की सीमाओं का निश्चित परिसीमन किया जाए, जिससे उनमें असामान्य रूप से वृद्धि न हो सके और कृषि-भूमि का भी अतिक्रमण रुक सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए, जिससे नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोका जा सके।
प्रश्न 3
कस्बों तथा नगर में क्या अन्तर है? [2014]
उत्तर
कस्बा (Town) कस्बा नगरीय गाँव की अपेक्षा एक बड़ी इकाई है। इसमें मकान सटे हुए, सड़कें तंग तथा गलियाँ सँकरी होती हैं। ये कस्बे सड़क मार्गों के संगम या रेलपथ पर स्थित होते हैं। इसके दो क्षेत्र होते हैं- आवासीय एवं व्यावसायिक। नगरों से इसका पृथक्करण जनसंख्या के आधार : पर किया जाता है। सामान्य रूप से इनकी जनसंख्या 5,000 से 10,000 व्यक्ति तक मानी गई है।
नगर (City) नगर उस क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ विशाल जनसमूह निवास करता है, जो समीपवर्ती क्षेत्र से अतिरिक्त उत्पादक वस्तुएँ एकत्रित करता है तथा आर्थिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्रिया-कलापों का केन्द्र होता है। 50 हजार से 10 लाख तक की जनसंख्या रखने वाली बस्ती को प्रायः नगर कहा जाता है। नगर अपने समीपवर्ती क्षेत्र से आर्थिक शक्ति ग्रहण कर तेजी से विकसित होते हैं। नगर वस्तुतः एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन होता है। नगरों के विकास का आधार उद्योग-धन्धे तथा व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं।
प्रश्न 4
नगरीय अधिवासों के दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। [2013, 14, 16]
उत्तर
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत नगरीय अधिवासों के प्रकार’ शीर्षक देखें।
प्रश्न 5
नगरीकरण से उत्पन्न किन्हीं चार समस्याओं का वर्णन कीजिए। [2010, 12, 13, 14]
उत्तर
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत नगरों की समस्याएँ या दोष’ शीर्षक देखें।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
जनसंख्या एवं नागरिक कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है?
उत्तर
जनसंख्या एवं नागरिक कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों को चार भागों में बाँटा जा सकता है-
- पुरवा या टोला
- नगरीय या बाजार गाँव
- कस्बा और
- नगर।
प्रश्न 2
खनन नगर से क्या अभिप्राय है?
उत्तर
खनिज पदार्थ वाले क्षेत्रों में ऐसे नगरों का विकास होता है। झारखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह और कर्नाटक का कोलार खनन नगर हैं।
प्रश्न 3
नगरीकरण से उत्पन्न किसी एक समस्या की विवेचना कीजिए। [2010]
उत्तर
नगरीकरण होने से जनसंख्या की अतिशय वृद्धि होती है जिससे नगरों के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा जनसंख्या की सघनता की समस्या हो जाती है। भूमि तथा भवनों के किराये बढ़ जाते हैं तथा भीड़ के कारण यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1
मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
(क) टेलर ने
(ख) जीन गोटमैन ने
(ग) डेविस ने
(घ) पेन्क ने
उत्तर
(ख) जीन गोटमैन ने।
![]()
प्रश्न 2
लिपिसे-कौन औद्योगिक नगर नहीं है ?
(क) र
(ख) सिन्द्री
(ग) रंग
(घ) पुणे
उत्तर
(घ) पुसी।
प्रश्न 3
सन्नगर नहीं हैं –
(क) पुणे
(ख) हावड़ा
(ग) गाजियाबाद
(घ) नैनी
उत्तर
(क) पुणे।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 9 Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Geography Chapter 9 Urban Settlements (नगरीय अधिवास बस्तियाँ), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.