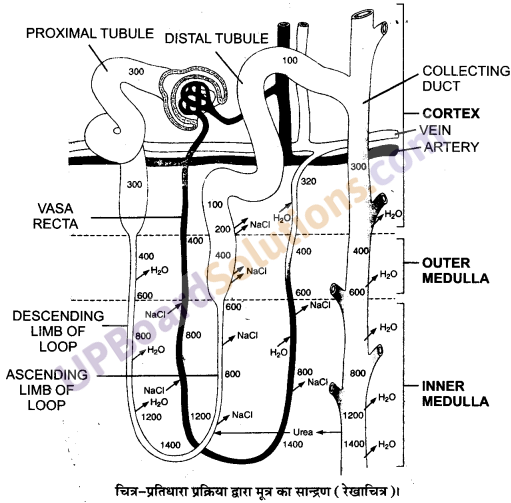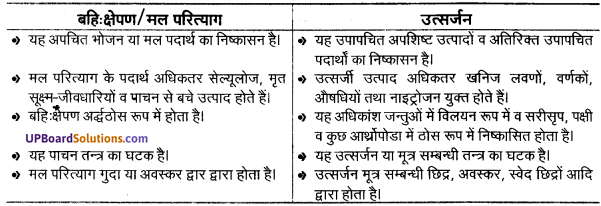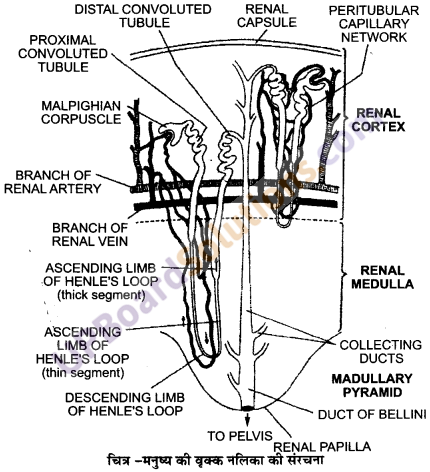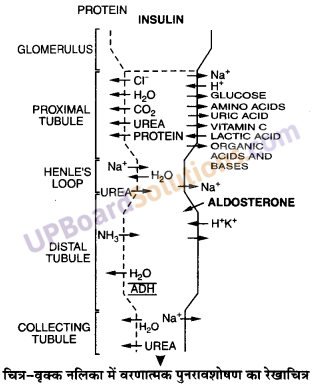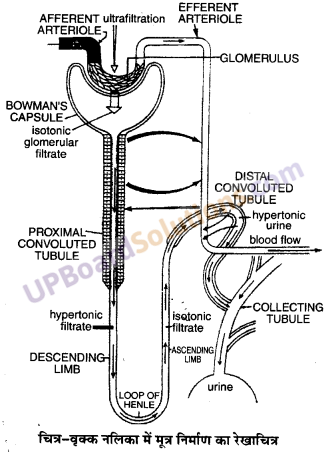UP Board Solutions for Class 11 Sociology Introducing Sociology Chapter 3 Understanding Social Institutions (सामाजिक संस्थाओं को समझना)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 11 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sociology Introducing Sociology Chapter 3 Understanding Social Institutions (सामाजिक संस्थाओं को समझना).
पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
ज्ञात करें कि आपके समाज में विवाह के कौन-से नियमों का पालन किया जाता है?
उत्तर
विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। यह यौन संतुष्टि एवं प्रजनन का समाज द्वारा मान्य तरीका है। विवाह द्वारा ही परिवार का निर्माण होता है। भारतीय समाज में विवाह में अनेक नियमों का पालन किया जाता है। इन नियमों का संबंध विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है, को नियंत्रित करने से है। वैधानिक रूप से भारत में एकविवाह के नियम का प्रचलन है। इस प्रकार के विवाह में एक व्यक्ति को एक समय में एक ही जीवनसाथी तक सीमित रहना पड़ता है। अर्थात् पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। जहाँ बहुविवाह की अनुमति है। (जैसे मुसलमानों में) वहाँ भी एकविवाह ही ज्यादा प्रचलित है। पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है। पहले भारत में उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं/विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी। इसका प्रचलन 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों के बाद ही हुआ।
परंपरागत रूप से भारत में जीवनसाथी के चयन का निर्णय अभिभावकों/संबंधियों द्वारा किया जाता रहा है। अब जीवनसाथी के चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाने लगी है। अंतर्विवाह का नियम व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक समूह (जैसे जाति) में ही विवाह की अनुमति देता है, जबकि बहिर्विवाह का नियम अपने समूह से बाहर (जैसे गोत्र से बाहर) विवाह करने पर बल देता है। उत्तरी भारत में गाँव-बहिर्विवाह का नियम भी प्रचलित है अर्थात् एक ही गाँव के लड़के एवं लड़की में विवाह नहीं हो सकता। पितृवंशीय व्यवस्था के नियम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियाँ अपने अभिभावकों के पास बार-बार न जाएँ। विवाह के नियमों में भिन्नता का पता आप अपनी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों से अपने प्रेक्षणों की तुलना करके भी लगा सकते हैं।
![]()
प्रश्न 2.
ज्ञात करें कि व्यापक सन्दर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार में सदस्यता, आवासीय प्रतिमान और यहाँ तक कि पारस्परिक संपर्क का तरीका कैसे परिवर्तित होता है?
उत्तर
भारत में परिवार के स्वरूपों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में अधिकतर यह मान लिया जाता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के परिणामस्वरूप एकाकी परिवारों में वृद्धि हो रही है। एकांकी परिवार भारतीय समाज के लिए नए नहीं हैं। भारत में अभावग्रस्त जातियों एवं वर्गों में इस प्रकार के परिवारों का अतीत में भी प्रचलन रहा है। परिवार में होने वाले परिवर्तन व्यापक संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से जुड़े हुए होते हैं। इसे प्रवसने के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जो व्यक्ति प्रवास कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं उनका परिवार, ग्रह, उसकी संरचना और मानक उसके परंपरागत समाज से भिन्न हो सकते हैं। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने परिवार एवं नातेदारी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आज नातेदारी से संबंधित विभिन्न परिवारों में पारस्परिक सम्पर्क कम होता जा रहा है। यह केवल सुख-दु:ख के समय तक ही सिमटने लगा है। परिवार के सदस्यों के संबंधों में भी औपचारिकता का अंश आने लगा है। 1990 के दशक में जर्मनी का एकीकरण यद्यपि एक राजनीतिक घटना है, तथापि इसका प्रभाव परिवार पर स्पष्ट देखा जा सकता है। नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएँ रद्द कर दी थीं। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इन्कार करने लगे।
प्रश्न 3.
कार्य पर एक निबंध लिखिए। कार्यों की विद्यमान श्रेणी तथा ये किस तरह बदलती हैं, दोनों पर ध्यान केंद्रित करें।
उत्तर
कार्य का संबंध भूमिका निष्पादन से हैं। प्रत्येक परिवार एवं गृह में कार्यों का स्पष्ट विभाजन विद्यमान होता है। कार्य स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का द्योतक है। कार्य की यह आधुनिक संकल्पना अत्यधिक सरलीकृत है क्योंकि बहुत-से कार्य सवेतन नहीं होते। उदाहरणार्थ-अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आँकड़ों में नहीं गिने जाते। नकद भुगतान के अतिरिक्त कार्य या सेवा के बदले वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान भी किया जाता है। भारत में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन इसी का द्योतक है। पूर्व आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग खेती में कार्य करते या पशुओं की देखभाल करते थे। औद्योगिक समाजों में छोटा भाग कृषि कार्यों में संलग्न होता है तथा स्वयं कृषि का औद्योगीकरण हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कृषि में भी मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य को मशीनों द्वारा किया जाने लगता है। सेवा क्षेत्र का विस्तार कार्यों में विविधता लाता है। इसीलिए अत्यधिक जटिल श्रम-विभाजन को आधुनिक समाजों का लक्षण माना जाता है। आधुनिक समाज में कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है। पहले कभी पूरा परिवार कार्य की इकाई माना जाता था, जबकि अब घर और कार्य एक-दूसरे से अलग हो गए हैं। उद्योगों में कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। पिछले कुछ दशकों से भूमंडलीकरण के कारण ‘उदार उत्पादन’ और ‘कार्य के विकेंद्रीकरण’ की तरफ झुकाव देखा जा सकता है।
कई बार कार्यों की विद्यमान श्रेणी में भी परिवर्तन स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ-जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्य का प्रबंध करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे अपने परिवार की एकमात्र भरण-पोषण करने वाली बन जाती हैं। दक्षिण-पूर्व महाराष्ट्र तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में इस प्रकार के परिवर्तनों से ही महिला-प्रधान घरों की संकल्पना का विकास हुआ है।
प्रश्न 4.
अपने समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें। वे आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं?
उत्तर
प्रारंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन अधिकारों को अधिकतर संघर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता था। राजतंत्र की शक्तियों को सीमित करना अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत करना इसी संघर्ष का परिणाम है। फ्रांस की क्रांति तथा भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस प्रकार के आंदोलनों के उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। भारत में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त है। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार रहने की जगह चुनने की, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार सम्मिलित है। राजनीतिक अधिकारों में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है तथा सार्वजनिक पद के लिए खड़ा हो सकता है। सामाजिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित जातियों को दिए गए विशेष अधिकार इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना भी व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार देना ही है।
अधिकार व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। समाज के बहुत-से वर्ग अन्य वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता भी इसी का ही परिणाम है। बहुत-से विकासशील देशों में सामाजिक अधिकारों को आर्थिक विकास से रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किए जाने लगे हैं तथा इन्हें प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया जाने लगा है।
![]()
प्रश्न 5.
समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है?
उत्तर
धर्म का संबंध अलौकिक शक्तियों पर विश्वास से है। यद्यपि धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है, तथापि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। धर्म के साथ अनेक अनुष्ठान जुड़े हुए होते हैं। प्रार्थना करना, गुणगान करने, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या न करना, उपवास रखना आदि आनुष्ठानिक कार्य ही है। समाजशास्त्र में धर्म का अध्ययन धार्मिक या ईश्वरमीमांसीय अध्ययन से भिन्न है। समाजशास्त्र की मुख्य रुचि यह ज्ञात करने में है कि धर्म समाज में कैसे कार्य करता है तथा अन्य संस्थाओं से इसका क्या संबंध है। विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा धर्म की भूमिका की समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। धर्म, धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं संस्थाएँ संस्कृति के अन्य पक्षों को जिस रूप में प्रभावित करती हैं इसे ज्ञात करने में भी समाजशास्त्रियों की विशेष रुचि होती है। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की रुचि धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन करने में नहीं है, अपितु इसे समाज की अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों के संदर्भ में ही देखा जाता है।
प्रश्न 6.
सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। अपनी पढ़ाई और वैयक्तिक प्रेक्षणों, दोनों का इसमें प्रयोग कीजिए।
उत्तर
शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती है। सीख के रूप में परिवार में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा जीवन-पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यालयों में प्रवेश लेना महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी से प्रारंभ होने वाली औपचारिक शिक्षा रोजगार प्राप्त करने की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है। शिक्षा द्वारा कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताएँ भी प्राप्त होती हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी तो उपलब्ध कराता ही है, साथ ही यह समूह की विरासत के प्रेषण/संप्रेषण की आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। आधुनिक समाजों मे श्रम के आर्थिक विभाजन के कारण औपचारिक शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया है। आज यह माना जाने लगा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए।
प्रश्न 7.
चर्चा कीजिए कि सामाजिक संस्थाएँ परस्पर कैसे संपर्क करती हैं।
उत्तर
सामाजिक संस्थाओं में परस्पर संपर्क एवं अंतक्रिया पाई जाती है। कोई भी संस्था शुन्य में कार्य नुहीं करती है। उदाहरणार्थ–धर्म की संस्था समाज में एकीकरण का महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य करती है तो शिक्षा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समाज की अर्थव्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करती है। मैक्स वेबर ने धर्म के अध्ययन में इसके पूँजीवाद नामक आर्थिक संस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन किया है। उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि ईसाई धर्म की कैल्विनवादी शाखा ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूँजीवाद के उद्भव एवं विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसी भाँति, धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। उदाहरणार्थ-इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय-समय पर सामाजिक परिवर्तन हेतु धार्मिक आंदोलन हुए हैं। जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। धर्म किसी व्यक्ति किसी निजी आस्था का मामला ही नहीं होता, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है। धर्म का यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण होता है।
क्रियाकलाप आधारित प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
लोगों द्वारा परिवार, धर्म, राज्य के लिए बलिदान देने के उदाहरणों के बारे में चर्चा कीजिए। (क्रियाकलाप 1)
उत्तर
लोगों में अपने परिवार, धर्म एवं राज्य के लिए निष्ठा कोई नहीं बात नहीं है। वे इनके लिए अपन हितों को अनदेखा करने तथा किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों का राज्य की रक्षा हेतु दुश्मनों के हाथों मारा जाना उनका राज्य के प्रति बलिदान ही दर्शाता हैं। अनेक धार्मिक संप्रदायों में अनेक धर्म-गुरुओं द्वारा अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने अथवा परिजनों के बलिदान के उदाहरण पाए जाते हैं। बहुत-से लोग अपने परिवार के आर्थिक हितों के सामने अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। इसके लिए वे परिवार छोड़ दूरदराज के क्षेत्रों में या विदेशों में नौकरी करने में भी संकोच नहीं करते हैं। क्षेत्रवाद की भावना भी अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा का ही परिणाम है। यह भावना विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्य के लोगों को कई बार आपस में लड़ने-मरने पर विवश कर देती है।
प्रश्न 2.
प्रसिद्ध कहावतों में समाज की सामाजिक व्यवस्था की झलक कैसे मिलती है? (क्रियाकलाप 2)
उत्तर
ऐसा माना जाता है कि कहावतों में समाज की सामाजिक व्यवस्था की झलक ही मिलती है। उदाहरणार्थ-लड़कियों को ‘पराया धन’ माना जाता है। इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अपने माता-पिता की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। परिवार में होने वाला यह लिंग-भेदभाव भारत सहित अनेक समाजों में संस्थागत रूप में विद्यमान रहा है। इससे संबंधित अनेक कहावतें भी विकसित हुई हैं। उदाहरणार्थ-एक तेलुगु कहावत है कि “एक लड़की का पालन करना दूसरे के आँगन में पौधे को पानी देने के बराबर है।” यह कहावत लड़कियों को पराया धन माने जाने को चरितार्थ करती है।
प्रश्न 3.
विभिन्न समाजों द्वारा विवाह के लिए साथियों की तलाश किए जाने वाले विभिन्न तरीकों का पता लगाइए। (क्रियाकलाप 3)
उत्तर
विभिन्न समाजों में विवाह के लिए जीवनसाथी की तलाश के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। पहले कभी हिन्दुओं में विवाह कराने में बिचौलियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। कुछ लोग लड़के या लड़की वालों को उपयुक्त जीवनसाथी के बारे में बताते थे। अब अनेक जातियाँ अपनी पत्रिकाएँ निकालने लगी हैं जिनमें वैवाहिक विज्ञापन दिए जाते हैं। प्रमुख समाचार-पत्रों में ऐसे वैवाहिक विज्ञापन आने लगे हैं। मुसलमानों में चूंकि नातेदारों में विवाह हो सकता है, इसलिए जीवनसाथी के चयन में नातेदारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनजातियों में जीवनसाथी के चयन के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। कठिन जीवन होने के कारण लड़कियाँ लड़कों की परीक्षा ले सकती हैं (परीक्षा विवाह); लड़के-लड़की को विवाह से पूर्व कुछ समय के लिए एक-दूसरे को समझने के लिए साथ रहने की अनुमति दी जा सक़ती थी (परिवीक्षा विवाह); लड़की के पिता को वधु-मूल्य देकर विवाह किया जा सकता (क्रय विवाह); लड़की को जबरदस्ती उठाकर विवाह किया जा सकता है (अपहरण विवाह); लड़की होने वाले पति के माता-पिता की सेवा द्वारा उन्हें विवाह के लिए राजी कर सकती है (सेवा विवाह); एक परिवार के लड़के-लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की-लड़के से विनिमय द्वारा हो सकता है (विनिमय विवाह); लड़का और लड़की परस्पर सहमति से विवाह कर सकते हैं। (सहपलायन विवाह) आदि।
प्रश्न 4.
शादी से संबंधित विभिन्न गीतों को इकट्ठा कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये किस तरह शादियों में सामाजिक परिवर्तनों और लिंग संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं? (क्रियाकलाप 4)
उत्तर
शादियों से संबंधित अधिकांश लोकगीत लड़की को पराया धन, उसकी विदाई के दु:ख अथवा उसके होने वाले संबंधियों को चित्रित करने वाले होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं-
1. पिताजी हम चिड़ियों के झुंड की तरह हैं।
हम दूर उड़ जाएँगी : और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी,
हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएँगी,
पिताजी, मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती,
(क्योंकि द्वार बहुत छोटा है)
बेटी, मैं एक ईंट निकाल दूंगा
(तुम्हारी पालकी के लिए द्वार बड़ा करने के लिए)
तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा।
2. मैं अपनी बच्ची को पालने में झुलाता हूँ, और
उसके सुंदर बालों में अँगुलियों फिरा रहा हूँ,
एक दिन दूल्हा आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा।
जोर से ढोल-नगाड़े बजते हैं।
और मधुर शहनाई बज रही है।
एक अजनबी का बेटा मुझे लेने आ गया है।
मेरी सहेलियों, अपने खिलौने लेकर आओ।
चलो हम खेलेंगी, क्योंकि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊँगी
जब मैं एक अजनबी के घर चली जाऊँगी।।
3. जमुन जल बरसे, हाय धीरे-धीरे
जमुन जल बरसे-2, गागर मोरी टपके हाय धीरे-2
गागर मोरी टपके-2, पैर मोरा फिसले हाय धीरे-2
पैर मोरा फिसले-2, सास मोरी मारे हाथ धीरे-2
सास मोरी मारे-2, ननद पिटवावे हाय धीरे-2
ननद पिटवावे-2, छज्जे पे ठाड़ों देखे हाय धीरे-2
छज्जे पे ठाड़ो देखे-2, तरस नहीं आवे धीरे-2
तरस नहीं आवे-2, मैं पीहर चली जाऊँगी हाय धीरे-2
मैं पीहर चली जाऊँगी-2, भइया पे बुलवाय लऊँ हाय धीरे-2
भइया पे बुलवाय लऊँ-2, बाबुल पे पिटवाऊँ हाय ‘धीरे-2
बाबुल पे पिटवाऊ लऊँ-2, तरस मोहे आवे हाय धीरे-2
तरस मोहे आवे-2, मैं फौरन छुड़वाऊँ हाय धीरे-2
मैं फौरन छुड़वा-2, मैं संग चली जाऊँ हाय धीरे-2
जमुन जल बरसे, हाय धीरे-धीरे।
प्रश्न 5.
क्या आप सोचते हैं कि अंतर्विवाह आज भी प्रचलित मानक है? (क्रियाकलाप 5)
उत्तर
अंतर्विवाह का अर्थ है अपने ही समूह में विवाह करना। भारतीय समाज में अंतर्विवाह के नियम स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जाति एक अंतर्विवाही समूह है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। फोलसम (Folsom) के अनुसार अंतर्विवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपनी जाति या समूह में विवाह करना पड़ता है यद्यपि निकट के रक्त संबंधियों में विवाह की अनुमति नहीं होती है। भारत में सभी जातियाँ तथा उपजातियाँ अंतर्विवाह हैं। अंतर्विवाह संबंधी निषेध हिंदुओं, मुसलमानों तथा जनजातियों में भी पाए जाते हैं। इस सब में यह पहले से ही निश्चित है। कि विवाह किनसे किया जा सकता है अर्थात् विवाह का क्षेत्र सीमित है। प्रजातीय भिन्नता तथा अपनी प्रजाति की शुद्धता बनाए रखना इस निषेध का प्रमुख कारण माना जाता है। यद्यपि अंतर्जातीय विवाहों के परिणामस्वरूप आज भारत में अंतर्विवाह का नियम थोड़ा-बहुत शिथिल होने लगा है, तथापि आज भी अधिकांशतया अंतर्विवाह ही एक प्रचलित मानक है। यदि हम वैवाहिक विज्ञापनों को देखें तो उनमें से अधिकांश में जाति का प्रतिबंध लिखा हुआ नहीं होता। इससे यह पता चलता है कि बहुत-से-लोग अब इस अंतर्विवाह के नियम को नहीं मानते हैं।
![]()
प्रश्न 6.
विवाह की पसंद को समझने में विज्ञापन आपकी कैसे सहायता करते हैं? (क्रियाकलाप 5)
उत्तर
प्रत्येक माता-पिता में अपने लड़के एवं लड़की अथवा स्वयं वर एवं वधू में जीवनसाथी में पाए। जाने वाले गुणों के बारे में कुछ प्राथमिकताएँ होती हैं। वैवाहिक विज्ञापनों में आज इस कार्य को सरल बना दिया है। अधिकांश वैवाहिक विज्ञापनों में वर एवं वधू के शारीरिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, जातीय एवं धार्मिक लक्षणों का वर्णन मिलता है। इनसे परिवार वाले या स्वयं लड़का या लड़की अपनी पसंद के जीवनसाथी का चयन कर उससे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। विज्ञापनों द्वारा होने वाले अनेक विवाह काफी सफल रहे हैं क्योंकि इनसे जीवनसाथी के चयन का दायरा बढ़ जाता है।
प्रश्न 7.
ग्राम आधारित व्यवसायों में लगे भारतीयों की संख्या की गणना कीजिए और उन व्यवसायों की एक सूची बनाइए। (क्रियाकलाप 6)
उत्तर
भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। 2011 ई० की जनगणना के अनुसार आज भी लगभग 62 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि भारत की एक-तिहाई जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है तथा रोजगार एवं आय के लिए अभी भी कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। कृषि क्षेत्र कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 22 प्रतिशत है। ग्रामीण परिवारों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे या तो कृषि से संबंधित होते हैं या कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय होते हैं। कृषि से संबंधित कार्यों में खेती करना तथा पशुओं की देखभाल करना प्रमुख हैं, जबकि कृषि से जुड़े कार्यों में परंपरागत जातिगत कार्य; जैसे लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, लोहे का काम करने वाले लोहार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार आदि को सम्मिलित किया जाता है। खेतिहर मजदूर भी कृषि में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुक्कुट एवं डेरी उद्योग में भी अनेक ग्रामवासी कार्यरत होते हैं। पारंपरिक समाजों में गैर-कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता था। पहले कभी ग्रामीण उद्योगों में भी काफी ग्रामवासी लगे हुए थे। अब लघु एवं कुटीर उद्योगों के हृास के कारण इनमें लगे लोगों की संख्या कम हुई है। वाइजर नामक समाजशास्त्री ने करीमपुर गाँव में जजमानी व्यवस्था पर किए गए, अध्ययन में वहाँ रहने वाली चौबीस जातियों के कार्यों का उल्लेख किया है। इनमें से अधिकांश जातियाँ अन्य जातियों को अपनी परंपरागत सेवाएँ प्रदान करती है। इनमें उन्होंने पुरोहित अथवा अध्यापक (ब्राह्मण); वंश परम्परा का वर्णन करने वाले (भाट); खजांची (कायस्थ); सोने का काम करने वाले (सुनार); फूल-पत्ती का प्रबंध करने वाले (माली); सब्जियाँ उगाने वाले (काछी); चावल उगाने वाले (लोधा); बढ़ईगिरी का काम करने वाले (बढ़ई); हजामत बनाने वाले (नाई); पानी लाने वाले (कहार); भेड़-बकरियाँ पालने वाले (गड़रिया); भाड़ में अनाज भूनने वाले (भड़पूँजा); कपड़े सिलने वाले (दर्जी); मिट्टी के बर्तन बनाने वाले (कुम्हार); व्यापार करने वाले (साहूकार या महाजन); तेल निकालने वाले (तेली); कपड़े धाने वाले (धोबी); मेट बनाने वाले (धानुक); चमड़े का काम करने वाले (चर्मकार); सफाईकर्मी; पैतृक मुसलमान भिखारी (फकीर); शीशे की चूड़ियाँ बेचने वाले (मनिहार); कपास धुनाई करने वाले (धुनक) तथा नाचने वाली लड़की (तवायफ) को सम्मिलित किया है।
प्रश्न 8.
हाल ही के वर्षों में क्या भारत में सेवा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है? ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं? ज्ञात कीजिए। (क्रियाकलाप 7)
उत्तर
भारत में पिछले कुछ दशकों में सेवा के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। 2011-12 ई० में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत 58.3 था। 2000 के दशक के पश्चात् कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की कीमत पर इस क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। इसका प्रमुख कारण सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रकियाएँ हैं। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास ने सेवा के क्षेत्र के विस्तार तथा घर एवं कार्य को अलग करने में योगदान दिया है। अब कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र-बिंदु बन गए हैं। उद्योगों में कार्य करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते हैं तथा उन्हें कार्य के बदले वेतन मिलता है। बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार तथा नौकरशाही के विकास ने दफ्तरों में नौकरियों की संख्या में वृद्धि की है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र का भी अत्यधिक विकास हुआ है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा एवं पर्यटन उद्योग का काफी विस्तार हुआ है। अब सेवा क्षेत्र में अधिकाधिक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं।
प्रश्न 9.
क्या आपने मुख्य बुनकर को कार्य करते देखा है? उसे एक शाल बनाने में कितना समय लगता है? ज्ञात करें। (क्रियाकलाप 8)
उत्तर
भारत में शाल बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। बुनकर बिना किसी अन्य परिजन की सहायता से दो दिन में एक शाल बना सकता है। यदि बुनकर लंबी अवधि तक कार्य करता है तथा परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी सहायता करते हैं तो वह एक दिन में एक शाल बना सकता है। बुनकर हैंडलूम द्वारा एक दिन में एक से अधिक शाल तथा पावरलूम द्वारा एक दिन में अनेक शाल बना सकता है। पावरलूम हेतु उसे बिजली की उपलब्धता पर भी आश्रित होना पड़ता है।
प्रश्न 10.
अपने खाने वाले भोजन, रहने वाले मकान में प्रयुक्त सामग्री और पहनने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। ज्ञात कीजिए कि इन्हें किसने और कैसे बनाया। (क्रियाकलाप 9)
उत्तर
खाने वाले भोजन में गेहूं, चावल, दालों, सब्जियों इत्यादि का उत्पादन कृषकों द्वारा किया जाता है। गाँव में भैंस एवं गाय पालन करने वाले अथवा डेरियाँ दुग्ध को उपलब्ध कराने के प्रमुख साधन हैं। मकान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में ईंट, सीमेंट, बालू, रोड़ी, बदरपुर, लकड़ी, लोहे, पत्थर/टाइल्स, सेनेटरी का सामान, शीशे इत्यादि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इन सबकी उपलब्धता विभिन्न स्रोतों द्वारा होती है। उदाहरणार्थ-ईंटें भट्टों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, सीमेंट एवं सेनेटरी का सामान व शीशे इत्यादि फैक्टरियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि बालू, रोड़ी, बदरपुर आदि इनसे संबंधित ठेकेदारों या दुकानदारों द्वारा उपलब्ध होते हैं। लकड़ी टिंबर व्यवसायियों के यहाँ से खरीदी जाती है। वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाला कपड़ा कपास, रेशम, ऊन इत्यादि से हैंडलूम पर या कारखानों में बनता है, फिर बाजार के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचता है तथा ग्राहक अपनी पसंद का कपड़ा खरीदकर दर्जी से अपना पहनावा तैयार कराते हैं।
![]()
प्रश्न 11.
पता लगाएँ कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। (क्रियाकलाप 10)
उत्तर
मताधिकार प्राप्त करने हेतु महिलाओं को सभी देशों में काफी प्रयास करना पड़ा है। महिला संगठनों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में राजनीतिक समता की माँग के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया में 1918 ई०, अमेरिका में 1920 ई०, कनाडा में 1940 ई०, लैटिन अमेरिकी देशों (मैक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वेडोर आदि) में 1953 ई०, अफ्रीका में 1994 ई०, एशिया में जापान में 1924, ई० तथा भारत में 1950 ई० में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। यूरोप में फिनलैंड में सबसे पहले 1906 ई० में, ब्रिटेन में 1918 ई० में, जर्मनी 1919 ई० में, स्वीडन में 1921 ई० में, फ्रांस में 1944 ई० में तथा इटली में 1945 ई० में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। कुवैत, सऊदी अरब, कतार, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, गुआना, हाँगकाँग, सूरीनाम तथा ताइवान जैसे देशों में अभी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। भूटान में परिवार का केवल एक सदस्य ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
प्रश्न 12.
संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग क्यों की जा रही है? ज्ञात कीजिए। (क्रियाकलाप 10)
उत्तर
सामाजिक संरचना में लिंग असमता के परिणामस्वरूप विकसित विसंगतियों को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि महिलाओं हेतु संसद जैसी सर्वोच्च संस्था में भी उचित प्रतिनिधित्व हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। भारत में स्थानीय निकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है। लिंग समता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संसद में भी महिलाओं के लिए यदि आधे स्थान सुरक्षित रखना संभव नहीं तो कम-से-कम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होना आवश्यक है। सरकार के बार-बार प्रयास करने के बाद भी अभी तक महिलाओं का आरक्षण संबंधी बिल पारित नहीं हो पाया है। सरकार सहमति के आधार पर यथाशीघ्र इसे पारित करने हेतु प्रयासरत है। इस आरक्षण से महिलाओं में न केवल राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी, अपितु उनके सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा।
प्रश्न 13.
क्या आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच कोई संबंध देख पाते हैं? (क्रियाकलाप 11)
उत्तर
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारी को लागू करने का दायित्व राज्य पर होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पश्चिमी समाजों में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों का पता चलता है। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्र में काफी अच्छी व्यवस्था थी। आजकल पूरे विश्व में सामाजिक अधिकारों को राज्य को उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं एवं संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। भूमंडलीकरण एवं निजीकरण जैसी आर्थिक प्रक्रियाओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनका लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं प्राप्त हो पाता है। प्रजाति, भाषा एवं धर्म पर आधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण का प्रभाव केवल राजनीतिक दलों पर ही नहीं पड़ता अपितु विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी पड़ता है जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। इससे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का पता चलता है।
प्रश्न 14.
ऐसी घटनाओं की सूचनाएँ एकत्रित करें जो सार्वभौमिक अन्तःसंबंधित विकास को दर्शाती हैं तथा साथ ही प्रजातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय मतभेदों को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं के बारे में भी सूचनाएँ एकत्रित करें। चर्चा कीजिए कि राजनीति और अर्थशास्त्र उनमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? (क्रियाकलाप 12)
उत्तर
सार्वभौमिक अन्त:संबंधित विकास को प्रभावित करने में राजनीति और अर्थशास्त्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरे विश्व में होने वाले महिला आंदोलन अथवा पर्यावरण संबंधी आंदोलन ऐसी घटनाएँ हैं जिनका संबंध विकास से है। विकास ने न केवल महिलाओं की समस्याओं के निराकरण में रुचि को बढ़ावा दिया है, अपितु पर्यावरणीय अवक्रमण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी महत्त्वपूर्ण बना दिया है। इन दोनों प्रकार के आंदोलनों की प्रकृति यद्यपि राजनीतिक है, तथापि इनके दूरगामी आर्थिक परिणाम भी हैं। अब यह सोचा जाने लगा है कि यदि आर्थिक विकास का लाभ लिंग असमानता को दूर नहीं कर पाता अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में आर्थिक विकास की कीमत देनी पड़ती है तो ऐसे आर्थिक विकास का क्या लाभ है? क्या ऐसा संभव नहीं है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ महिलाओं में भी आर्थिक स्वावलंबने बढ़े तथा पर्यावरण का अवक्रमण भी न हो? राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों में इस प्रकार के मुद्दों की प्राथमिकता राजनीति और अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है।
प्रश्न 15.
कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सोचकर बताइए। (क्रियाकलाप 13)
उत्तर
विद्यालयों के पाठ्यक्रमों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे बच्चों के एक विद्यालय के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस अध्ययन से पता चलता है कि बच्चों ने यही सीखा कि कार्य संबंधित क्रियाकलाप खेल संबंधित क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। कार्य संबंधित क्रियाकलापों में कोई भी या अध्यापक द्वारा निर्देशित सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। विद्यालय में होने वाला शिक्षण कार्य अनिवार्य होता है। खाली समय के क्रियाकलापों को खेल कहा जाता है। आज इस धारणा में परिवर्तन हो रहा है तथा शारीरिक शिक्षा व खेलकूद को सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाने लगा है। साथ ही, स्कूलों के पाठ्यक्रमों को इस प्रकार का बनाए जाने पर जोर दिया जाने लगा है जो मनोरंजक हों तथा बच्चे खेल-खेल में ही बहुत कुछ सीख जाएँ।
परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक संस्था का अर्थ है।
(क) अधिक लोगों का साथ-साथ रहना
(ख) कार्य करने का निश्चित ढंग
(ग) बड़ा सामाजिक समूह
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर
(ख) कार्य करने का निश्चित ढंग
प्रश्न 2.
निम्नलिखित में कौन-सी संस्था है ?
(क) मानव-समाज
(ख) दुकान
(ग) महाविद्यालय
(घ) राष्ट्र
उत्तर
(ग) महाविद्यालय
प्रश्न 3.
सामाजिक संस्था की विशेषता है।
(क) सदस्यता
(ख) अस्थायी प्रकृति
(ग) अमूर्त प्रकृति
(घ) औपचारिक नियंत्रण
उत्तर
(ग) अमूर्त प्रकृति
प्रश्न 4.
वह प्रथा, जिसमें स्त्री एक समय पर एक से अधिक पुरुषों से विवाह संबंध स्थापित कर सकती है, कहलाती है-
(क) बहुपत्नी विवाह
(ख) बहुपति विवाह
(ग) एक विवाह
(घ) समूह विवाह
उत्तर
(ख) बहुपति विवाह
![]()
प्रश्न 5.
वह प्रथा, जिसके अनुसार कोई भी पुरुष एक समय में एकाधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, कहलाता है-
(क) समूह विवाह
(ख) एक विवाह
(ग) बहुपति विवाह
(घ) बहुपत्नी विवाह
उत्तर
(घ) बहुपत्नी विवाह
प्रश्न 6.
बहिर्विवाह का तात्पर्य है-
(क) गोत्र के बाहर विवाह
(ख) प्रवर के बाहर विवाह
(ग) पिण्ड के बाहर विवाह
(घ) ये सभी
उत्तर
(घ) ये सभी
प्रश्न 7.
बहिर्विवाह निषेध के अंतर्गत निषेध लिखिए-
(क) जाति
(ख) गाँव
(ग) गोत्र
(घ) प्रजाति
उत्तर
(ग) गोत्र
प्रश्न 8.
अंतर्विवाह का नियम है-
(क) अपनी जाति के बाहर विवाह
(ख) अपनी जाति में विवाह
(ग) एक-विवाह
(घ) बिना दहेज विवाह
उत्तर
(ख) अपनी जाति में विवाह
प्रश्न 9.
“विवाह स्त्री और पुरुष के-फरिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है।” यह किसका कथन है ?
(क) बोगास
(ख) वेस्टरमार्क
(ग) पी० वी० यंग
(घ) देसाई
उत्तर
(क) बोगार्ड्स
प्रश्न 10.
निम्नलिखित में से हिन्दू विया की विशेषता कौन-सी है ?
(क) सामाजिक समझौता
(ख) धार्मिक संस्कार
(ग) अस्थायी संबंध
(घ) बिना अदालत तलाक
उत्तर
(ख) धार्मिक संस्कार
प्रश्न 11.
हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन-सा अप्रशस्त है?
(क) दैव
(ख) प्राजापत्य
(ग) राक्षस
(घ) ब्राह्म
उत्तर
(ग) राक्षस
प्रश्न 12.
वर्तमान समय में हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित प्रकार लिखिए
(क) ब्राह्म विवाह
(ख) दैव विवाह
(ग) गांधर्व विवाह
(घ) राक्षस विवाह
उत्तर
(क) ब्राह्म विवाह
प्रश्न 13.
यह कथन किसका है ‘धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है?
(क) मैकाइवर
(ख) डेविस
(ग) पैरेटो
(घ) टॉयलर
उत्तर
(घ) टॉयलर
![]()
प्रश्न 14.
धर्म की विशेषता क्या है ?
(क) पारस्परिक सहयोग
(ख) समानता
(ग) अलौकिक शक्ति पर विश्वास
(घ) गुरु पर विश्वास
उत्तर
(ग) अलौकिक शक्ति पर विश्वास
प्रश्न 15.
निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता नहीं है
(क) पवित्रता
(ख) आदर
(ग) विश्वास
(घ) सदाचार
उत्तर
(घ) सदाचार
प्रश्न 16.
निम्नलिखित में धर्म की विशेषता नहीं है-
(क) कर्मकाण्डों का समावेश
(ख) अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास
(ग) तर्क का समावेश
(घ) अपरिवर्तनशील व्यवहार
उत्तर
(ग) तर्क का समावेश
निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
परिवार सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार का साधन है?
उत्तर
परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है।
प्रश्न 2.
अंतर्विवाह क्या है?
उत्तर
विशिष्ट जाति, वर्ग या जनजातीय समूह के अंतर्गत किए जाने वाले विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं।
प्रश्न 3.
बहिर्विवाह क्या है?
उत्तर
संबंधी के कुछ समूहों के बाहर किए जाने वाले विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं।
प्रश्न 4.
पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-बहन इत्यादि किस प्रकार के नातेदार हैं?
उत्तर
पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-बहन इत्यादि प्राथमिक नातेदार हैं।
प्रश्न 5.
दो संबंधियों में प्रत्यक्ष संबंध एवं अंतःक्रिया को सीमित करने वाली नातेदारी रीति कौन-सी है?
उत्तर
दो संबंधियों में प्रत्यक्ष संबंध एवं अंत:क्रिया को सीमित करने वाले नातेदारी रीति का नाम परिहार है।
प्रश्न 6.
जिन नातेदारों में प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
उत्तर
जिन नातेदारों में प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिक नातेदार कहा जाता है।
प्रश्न 7.
ऐजूकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है?
उत्तर
‘ऐजूकेशन’ शब्द लैटिन भाषा के ‘ऐजूकेयर’ शब्द से बना है।
प्रश्न 8.
स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को क्यों कहा जाता है?
उत्तर
स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा’ कहा जाता है।
प्रश्न 9.
पवित्र और अपवित्र की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम लिखिए।
उत्तर
पवित्र और अपवित्र की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम दुखम है।
![]()
प्रश्न 10.
‘ऐलीमेण्टरी फॉर्स ऑफ रिलिजियस लाइफ’ नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए।
उत्तर
‘ऐलीमेण्टरी फॉर्स ऑफ रिलिजियस लाइफ’ नामक पुस्तक के लेखक का नाम दुर्चीम है।।
प्रश्न 11.
शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं?
उत्तर
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
परिवार किसे कहते हैं।
उत्तर
परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजी, पुत्र-पुत्री आदि सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं परंतु परिवार का यह रूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है। पाश्चात्य देशों में परिवार का तात्पर्य समाज की उस इकाई से लगाया जाता है जिसमें माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। इलियट तथा मैरिल (Elliott and Merrill) के अनुसार, “परिवार को पति-पत्नी तथा क्च्चों की एक जैविक-सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।” इनके अनुसार यह एक सामाजिक संस्था और एक सामाजिक संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
प्रश्न 2.
नातेदारी के दो प्रमुख भेद बताइए।
उत्तर
नातेदारी के दो प्रमुख भेद इस प्रकार हैं-
- विवाह संबंधी नातेदारी–इसमें हम उन सब नातेदारों को सम्मिलित करते हैं जो विवाह के संबंध के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ–एक स्त्री अपने पति अथवा एक पति का अपनी पत्नी से संबंध अथवा पति-पत्नी, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, ननदोई, मौसा, साढ़, पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि रिश्तेदारों को विवाह संबंधी नातेदारों में सम्मिलित किया जा सकता है।
- रक्त संबंधी नातेदारी-इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है तो समान रक्त के | संबंध के आधार पर एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ-भाई-बहन, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी इत्यादि को इस श्रेणी में रखा जाता है।
प्रश्न 3.
पूँजीवाद की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
पूँजीवाद में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं-
- पूँजीवाद में निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। निजी संपत्ति चाहे चल हो या अचल उस पर निजी अधिकार होता है, उसे छीनने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं होता है।
- पूँजीवाद में प्रतिस्पर्धा प्रमुख संस्था है। श्रमिक, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है।
प्रश्न 4.
साम्यवाद की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- इसमें निजी संपत्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है अपितु संपत्ति पर राज्य के अधिकार को अर्थात् सार्वजनिक अधिकार को अधिक मान्यता दी जाती है।
- साम्यवाद, श्रम को अत्यधिक महत्त्व देता है और इसमें व्यक्ति को पद उसकी कार्यकुशलता के आधार पर दिया जाता है।
प्रश्न 5.
सहकारी समाजवाद से क्या अभिप्राय है?
उत्तर
सहकारी समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें कुछ लोग सहयोग द्वारा कोई कार्य करते हैं। ये लोग श्रमिक भी होते हैं और लाभ पाने वाले सदस्य भी। उदाहरण के लिए–100 व्यक्तियों ने पूँजी लगाकर एक कारखाना खोला, ये व्यक्ति वहाँ के कार्यकर्ता भी होंगे तथा जो लाभ होगा वह इन व्यक्तियों में समान रूप से बाँट लिया जाएगा। सहकारी समाजवाद में घनिष्ठ आर्थिक संबंध, सहकारिता, सामूहिक संपत्ति आदि प्रमुख आर्थिक संस्थाएँ हैं। सहकारी समाजवाद का विकसित रूप इंग्लैंड तथा स्केण्डिनेवियन देशों में पाया जाता है।
![]()
प्रश्न 6.
संपत्ति की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
संपत्ति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं-
- संपत्ति एक सार्वभौमिक आर्थिक संस्था है। यह बिल्कुल ही आदिम समाज से लेकर अत्यधिक विकसित समाजों-सभी में पाई जाती है।
- संपत्ति की अवधारणा सीमित और मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार में निहित होती है। यह अधिकार संबंधित वस्तुओं पर नियंत्रण के विभिन्न रूपों को प्रकट करता है; जैसे–कब्जा, उपयोग, भोग, आय, वितरण आदि। सीमित और मूल्यवान वस्तुएँ दो प्रकार की हो सकती ” है—मूर्त तथा अमूर्त।।
प्रश्न 7.
जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा की परिभाषा दीजिए।
उत्तर
कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शक्तियाँ जन्मजात रूप से ही विद्यमान होती हैं परंतु इन शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, ये प्रयास ही शिक्षा हैं। इस मत के मुख्य समर्थक सुकरात, फ्रोबेल तथा विवेकानंद आदि हैं। सुकरात के अनुसार, “शिक्षा का आशय सार्वजनिक प्रामाणिकता के विचारों को प्रकाश में लाना है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रच्छन्न रूप में निहित हैं। इसी प्रकार फ्रोबेल के अनुसार, “शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है।”
प्रश्न 8.
धर्म किसे कहते हैं?
या
धर्म से आप क्या समझते हैं?
उत्तर
‘धर्म’ को अंग्रेजी में रिलीजन’ (Religion) कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ‘rel (I) igio’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ‘बाँधना’। इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में ‘धर्म’ का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक-दूसरे से बाँधते या जोड़ते हैं। अन्य शब्दों में, धर्म मनुष्य की युगों से विद्यमान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान के प्रति होती है। टायलर के अनुसार, “आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएँ दैवी तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं।”
प्रश्न 10.
पारिवारिक विघटन को परिभाषित कीजिए।
उत्तर
मार्टिन न्यूमेयर के शब्दों में, “पारिवारिक विघटन का अर्थ एकता तथा निष्ठा को भंग होना, पहले से स्थापित संबंधों की समाप्ति, पारिवारिक चेतना का नाश अथवा अलगाव का विकास है।”
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
परिवार को नागरिकता का प्रशिक्षण स्थल क्यों कहा जाता है।
उत्तर
मैजिनी के अनुसार, “बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के मध्य सीखता है। परिवार बालक में अनेक नागरिकता के गुणों का विकास करता है। इस संबंध में परिवार के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं-
- स्नेह की शिक्षा-स्नेह की शिक्षा बालक सर्वप्रथम माता के चुंबन और माता के दुलार से सीखता है। टी० रेमण्ट का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि “घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। माता-पिता का स्नेह बालक में भी प्रेम के बीज डाल देता है। बालक भी अपने माता-पिता से प्रेम करना सीख जाता है। भविष्य में यही पारिवारिक प्रेम व्यापक होकर सामाजिक प्रेम में परिणत हो जाता है।
- सहयोग की शिक्षा-सामाजिक जीवन में सहयोग का विशेष महत्त्व है। सामाजिक जीवन का आधार सहयोग ही है। बालक सहयोग का प्रथम पाठ परिवार में ही पढ़ता है; क्योंकि वह देखता है कि परिवार के समस्त सदस्य मिल-जुलकर घर का कार्य करते हैं। विद्वान् बोसो के अनुसार, “परिवार वह स्थान है, जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का यह नया पाठ सीखती है। कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता।”
- सहानुभूति की शिक्षा-परिवार में माता-पिता बालक के दुःख को देखकर तुरंत चितिंत हो उठते हैं और दौड़-भाग कर उसके दुःख को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी सच्ची सहानुभूति का प्रदर्शन बालक पर गहरा प्रभाव डालता है और वह भी समय पड़ने पर परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है।
- कर्त्तव्यपालन और आज्ञापालन की शिक्षा–आज्ञपालन और कर्तव्यपालन की शिक्षा भी बालक परिवार में ही सीखता है। प्रत्येक बालक अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। इस प्रकार वह अनुशासन का पाठ सीखता है।
- नि:स्वार्थता की शिक्षा–माता-पिता अपने बालक से नि:स्वार्थ प्रेम करते हैं और उनका लालन-पालन किसी स्वार्थ की भावना से नहीं करते। इससे परिवार के सदस्यों में नि:स्वार्थता के गुण का विकास होता है।
प्रश्न 2.
विवाह-प्रणाली के आधार पर परिवार को किन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है?
उत्तर
विवाह-प्रणाली के आधार पर परिवार को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–
- एकविवाही परिवार इस प्रकार के परिवार में पुरुष केवल एक ही विवाह करता है। आजकल इस प्रकार के परिवारों का ही अधिक प्रचलन है। ईसाइयों और यहूदियों में अतीतकाल में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
- बहुपत्नी परिवार—जिस परिवार का पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रखता है वह बहुपत्नी ‘ परिवार कहलाता है।
- बहुपति परिवार-इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। हमारे देश में टोडा और खस जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते है। चकराता में निवास करने वाली खस जनजाति में सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है।
![]()
प्रश्न 3.
अंतर्विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं? समझाइए।
उत्तर
अंतर्विवाह का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह, वर्ण या जाति के अंदर ही विवाह करना। प्राचीनकाल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था अतः लोग सामान्यतया अपने वर्ण में ही विवाह करते थे, परंतु धीरे-धीरे अनेक जातियों का विकास हो गया और लोग अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करने लगे। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में गौड़ ब्राह्मण केवल गौड़ ब्राह्मणों में ही विवाह करते हैं। इस प्रकार अंतर्विवाह एक ऐसी वैवाहिक मान्यता है जिसमें एक स्त्री अथवा पुरुष को अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करने का नियम होता है। अन्य शब्दों में, हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर विवाह करने का निषेध हैं। इसी निषेधु के पालन के लिए अंतर्विवाही समूहों का निर्माण किया गया। जाति प्रथा की परिभाषा के अनुसार, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। इस प्रकार के निषेधों का प्रमुख प्रजातीय शुद्धता, रक्त की शुद्धता तथा जातीय संगठन को दृढ़ बनाने की इच्छा प्रमुख रहे हैं। यद्यपि आज अधिकांशतया अंतर्विवाही मान्यताओं का पालन तो किया जाता है, तथापि अंतर्जातीय विवाहों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- शिक्षा के प्रसार ने जनसाधारण को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कर दिया है।
- सह-शिक्षा के प्रसार एवं युवक-युवतियों के पारस्परिक संपर्क ने विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है।
- दहेज प्रथा के दोषों के कारण।
- औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण दृष्टिकोण के व्यापक होने का परिणाम।
- यातायात के साधनों के विकास के कारण।
- व्यावसायिक कार्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्त्री-पुरुषों का साथ-साथ काम करना।
- युवक व युवतियों में स्वयं जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्र प्रवृत्ति।।
- विभिन्न सामाजिक सुधारों के प्रभाव।
प्रश्न 4.
नातेदारी की प्रमुख श्रेणियाँ कौन-सी हैं?
उत्तर
नातेदारी की श्रेणियों से अभिप्राय नातेदारों में परस्पर संबंधों की निकटता से है अर्थात् कोई नातेदार किसी व्यक्ति का कितना नजदीकी अथवा दूर का नातेदार है। नातेदारी को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है-
- प्राथमिक नातेदार–जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा प्रत्यक्ष वैवाहिक या रक्त संबंध होता है, उन्हें हम प्राथमिक नातेदार कहते हैं। प्राथमिक नातेदारों में आठ संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। ये हैं–पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्री, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, छोटे-बड़े भाई, छोटी-बड़ी बहन तथा भाई-बहन। ये वे प्रत्यक्ष संबंधी हैं जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है।
- द्वितीयक नातेदार—इसमें हम उन रिश्तेदारों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ये संबंधी हमसे प्राथकमिक संबंधियों द्वारा संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ-बहनाई-साले में संबंध, दादा-पोते में संबंध, चाचा-भतीजे में संबंध, देवर-भाभी में संबंध इस श्रेणी के संबंधों के उदाहरण हैं। मरडोक (Murdock) ने 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार बताए हैं।
- तृतीयक नातेदार–इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं अर्थात् हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। उदाहरणार्थ-साले की पत्नी, साले का लड़का, पड़दादा हमारे तृतीयक नातेदार हैं। मरडोक ने 151 ऐसे संबंधियों का उल्लेख किया है।
इसी प्रकार हम चातुथिक, पांचमिक इत्यादि संबंधों की चर्चा करते हैं।
प्रश्न 5.
हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियम को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
बहिर्विवाह का तात्पर्य है अपने रक्त-समूह आदि के अंतर्गत आने वाले सदस्य से विवाह न करना। इस मान्यता के अनुसार विवाह अपने गोत्र, प्रवर और सपिंड वाले परिवारों में नहीं किया जा सकता। हिंदुओं में तीन प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन है-
- गोत्र बहिर्विवाह-गोत्र बहिर्विवाह को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि ‘गोत्र के अर्थ को समझा जाए। मजूमदार एवं मदन के शब्दों में, ‘एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंश-समूहों को योग होता है, जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं। यह पूर्वज मानव, मानव के समान पश, पेड़, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है।’ गोत्र के संबंध में यह प्रथा प्रचलित है कि एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच में निकट रक्त-संबंध होते हैं। इसलिए एक ही गोत्र के सभी युवक-युवतियाँ एक-दूसरे के भाई-बहन हैं। अतः सगोत्र अथव अंत:गोत्र विवाहों पर प्रतिबंध हैं; क्योंकि हिंदू समाज में भाई-बहन के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकते।।
- सपिंड बहिर्विवाह–पिंड का अर्थ रक्त-संबंध से है। हिंदू समाज में सपिंड’ में वैवाहिक संबंध का निषेध किया गया है। सपिंड का संबंध माता की ओर से पाँच पीढ़ियों तक और पिता की ओर से सात पीढ़ियों तक माना जाता है। विज्ञानेश्वर ने सपिंड की व्याख्या इस प्रकार की है, एक ही पिंड अर्थात् एक देह से संबंध रखने वालों में शरीर के अवयव समान रहने के कारण सपिंड संबंध होता है। पिता और पुत्र सपिंड है। इसी प्रकार दादा आदि के शरीर के अवयव पिता द्वारा पोते में आने से तथा पुत्री की माता के साथ सपिंडता होती है; अतः जहाँ-जहाँ ‘सपिंड’ शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ एक शरीर के अवयवों का संबंध समझना चाहिए। इस प्रकार, पिता से सात और माता से पाँच पीढ़ी के बीच लड़के और लड़कियों में विवाह नहीं हो सकता।
- प्रवर बहिर्विवाह-प्रवर’ शब्द का अर्थ है ‘आह्वान करना। वैदिक काल में पुरोहित जिस समय अग्नि प्रज्वलित करते थे, उस समय अपने ऋषि-पूर्वजों का नाम लेते थे। आगे चलकर एक ऋषि का आह्वान करके यज्ञ करने वाले व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे को संबंधी समझने लगे। यह सत्य है कि ये संबंध धार्मिक भावना पर आधारित थे, परंतु इस पर भी वे अपने को एक वंश का सदस्य समझने लगे। ये सभी सदस्य प्रवर माने जाने लगे और उनमे आपस में विवाह संबंध का निषेध हो गया।
प्रश्न 6.
राजनीतिक संस्थाओं का क्या महत्त्व है?
उत्तर
राजनीतिक संस्थाओं की समाज तथा व्यक्तियों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भमिका होती है। राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था के रूप में राज्य की एक प्रमुख प्रकार्यात्मक समस्या लक्ष्य-प्राप्ति का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। राज्य तथा सरकार द्वारा केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किए जाते अपितु इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनिवार्य साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। राजनीतिक संस्थाएँ ही समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। राज्य, सरकार तथा कानून के डर से ही सभी नागरिक सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते हैनको राज्य दंडित करता है। राज्य एक सर्वशक्तिशाली संस्था है तथा इसे व्यक्ति का जीवन लेने अर्थात् उसे मृत्युदंड तक देने का अधिकार प्राप्त होता है। आर्थिक साधनों की प्राप्ति हेतु होने वाली होड़ को भी राजनीतिक संस्थाएँ ही नियमित करती है। शैक्षिक उप-व्यवस्था एवं अन्य उप-व्यवस्थाओं को दिशा-निर्देश देने का कार्य भी ” राजनीतिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था तथा इसकी निरंतरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
प्रश्न 7.
राजनीतिक संस्थाएँ क्या हैं?
उत्तर
राजनीतिक संस्थाओं का वृहद् अध्ययन राजनीतिशास्त्र में किया जाता है। चूंकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों को अध्ययन करता है, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। राजनीतिक संस्थाओं का संबंध शक्ति के वितरण से हैं तथा इनके द्वारा ही समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है और यदि सभी व्यक्ति ऐसा करने लगे तो सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। शांति तथा नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का महत्त्व सभी युगों में रहा है और आज भी है। व्यक्ति रांजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में व्यवस्था, प्रगति व शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्थाओं एवं समितियों पर ही हैं।
बॉटोमोर के अनुसार राजनीतिक संस्थाएँ समाज में शक्ति के वितरण से संबंधित हैं। इस संदर्भ में, राज्य के बारे में वेबर का विचार है कि राज्य एक ऐसा मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा में भौतिक बेल के वैधानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है और जो इस अधिकार से सफलतापूर्वक लागू करता है। इस प्रकार, राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण अभिकरण है। जिसके कार्य कानून द्वारा किए जाते हैं। राज्य संपूर्ण समाज नहीं है अपितु समाज की एक संस्था मात्र है।
![]()
प्रश्न 8.
आर्थिक संस्थाएँ क्या हैं?
उत्तर
मानव के जन्म के साथ ही उसे अनेक आवश्यकताएँ घेर लेती हैं। इनमें से कुछ आवश्यकताएँ उसकी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं; जैसे कि भोजन, वस्त्र तथा निवास की; और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ उत्पादन, विनिमय, वितरण से संबंधित होती है। आर्थिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। आर्थिक संस्थाएँ मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करती हैं। यदि मानवीय आवश्यकताएँ; विशेषकर भौतिक आवश्यकताएँ बिना नियमों के संघर्ष से प्राप्त होने की स्थिति में आ जाएँ तो सामाजिक संरचना ही नष्ट हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों को मत है कि आर्थिक संस्थाओं को समाज में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। यहाँ पर आर्थिक संस्था व आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि ‘आर्थिक व्यवस्था’ एक विस्तृत धारणा है, जबकि ‘आर्थिक संस्था’ सीमित धारणा है।
आर्थिक संस्थाओं का संबंध समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या से होता है। इनमें उने संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो समाज में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होती है। आर्थिक संस्थाओं द्वारा ही जीवन निर्वाह से सबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रमुख विद्वानों ने आर्थिक संस्था की परिभाषाएँ निम्नांकित प्रकार से दी हैं-
- एण्डरसन एवं पार्कर (Aderson and Parker) के अनुसार-“वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के माध्यम से आर्थिक संस्थाएँ समाज के अस्तित्व को बनाए रखती हैं। यह कार्य पूँजी, श्रम, भूमि, कच्चे माल तथा व्यवस्था संबंधी योग्यता के अधिकतम उपयोग द्वारा सम्भव होता है।
- डेविस (Davis) के अनुसार-समाज चाहे सभ्य हो या असभ्य, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत विचारों, आदर्श नियमों तथा पदों को आर्थिक संस्था की संज्ञा दी जाएगी।
प्रश्न 9.
आर्थिक संस्थाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
किसी भी समाज में आर्थिक संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः आर्थिक संस्थाएँ किसी समाज की उस प्रकार्यात्मक उप-व्यवस्था का निर्माण करती हैं जो समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या को हल करती है। इसलिए अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संस्थाओं को कई बार अनुकूलनकारी उप-व्यवस्था भी कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में लगी सभी इकाइयों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का कार्य आर्थिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्हीं से ऐसी सुविधाएँ उत्पन्न होती हैं जो सामान्य रूप से परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि के लिए आवश्यक होती है। इन्हीं संस्थाओं द्वारा कोई भी समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करता है तथा प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है।
आर्थिक संस्थाओं की प्रकृति एवं पूर्व-औद्योगिक तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। पूर्व-औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भूमि ही धन का स्रोत होती है, जीवंत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग होता है, सरल प्रौद्योगिकी पायी जाती है, श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण का निम्न स्तर पाया जाता है, प्रत्यक्ष एवं परंपरागत विनिमय तथा वितरण द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा अधिकतर प्रबंध का आधार परिवार ही होता है। इसलिए इन समाजों में संपत्ति तथा विनिमय संबंधी आर्थिक संस्थाओं की ही प्रमुखता होती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था आर्थिक संस्थाएँ विकसित श्रम-विभाजन, उत्पादन, व्यापार एवं लाभ तथा अप्रत्यक्ष विनिमय व वितरण से संबंधित होती है क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इन्हीं विशेषताओं की प्रमुखता पायी जाती है। समाज की विभिन्न उप-व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य साधने आर्थिक उप-व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इस उप-व्यवस्था, जिसमें आर्थिक संस्थाएँ भी सम्मिलित होती हैं, की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
प्रश्न 10.
संपत्ति की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
संपत्ति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं-
- संपत्ति एक सार्वभौमिक आर्थिक संस्था है। यह बिल्कुल ही आदिम समाज से लेकर अत्यधिक विकसित समाजों-सभी में पायी जाती है।
- संपत्ति की अवधारणा सीमित और मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार में निहित होती है। यह अधिकार संबंधित वस्तुओं पर नियंत्रण के विभिन्न रूपों को प्रकट करता है; जैसे—कब्जा, उपयोग, भोग, आय, वितरण आदि। सीमित और मूल्यवान वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं-मूर्त तथा अमूर्त।
- संपत्ति में उसके विषय में किसी अन्य पक्ष से सौदा कर सकने की क्षमता का तत्त्व मौजूद होता
- संपत्ति में हस्तांतरण किए जाने की क्षमता का होना भी आवश्यक है।
- संपत्ति एक आर्थिक तथ्य ही नहीं है वरन् एक सामाजिक तथ्य भी है। समाज ही संपत्ति अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और समाज ही उन अधिकारों का सीमांकन करता है। समाज की स्वीकृति के बिना संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है।
- अंत में, यह भी कहा जा सकता है कि संपत्ति अधिकार से आशय सदैव स्वामित्व के अधिकार से नहीं है। संपत्ति अधिकार वस्तु पर नियंत्रण से भी संबंधित है। इसलिए स्वामित्व और वस्तु के उपयोग का अधिकार समांतर रूप में दो प्रकार की संपत्तियों को प्रकट करता है।
प्रश्न 11.
पूँजीवाद की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
पूँजीवाद में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं-
- पूँजीवाद में निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। निजी संपत्ति चाहे चंल हो या अचल, उस पर निजी अधिकार होता है, उसे छीनने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं होता है।
- पूँजीवाद में प्रतिस्पर्धा प्रमुख संस्था है। श्रमिक, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों में प्रतिस्पर्धा पायी जाती है।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का कथन है कि समाज दो भागों में विभाजित होता है-
- पूँजीपति, जिनका कि आर्थिक साधनों पर पूर्ण अधिकार होता है तथा
- श्रमिक, जिनके पास केवल बेचने के लिए श्रम होता है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता है जिसे मार्क्स ‘वर्ग संघर्ष’ कहते हैं।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और अनेक श्रमिक काम करते हैं।
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। इस कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मजूदर संघों का निर्माण किया जाता है। ये मजदूर संघ श्रमिकों को सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
![]()
प्रश्न 12.
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
‘शिक्षा का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ-हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द ‘शिक्षा’ वास्तव में संस्कृत भाषा से लिया गया है तथा संस्कृत भाषा में इसका संबंध ‘शिक्षा’ धातु से है। संस्कृत भाषा में इस धातु का आशय ‘ज्ञान ग्रहण करने या विद्या प्राप्त करने से है। इस व्युत्पत्तिमूलक अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त करने या प्रदान करने की माध्यम है। अनेक विद्वान शिक्षा के इसी अर्थ को स्वीकार करते हुए शिक्षा की व्याख्या एवं व्यवस्था करने के पक्ष में हैं।
‘Education’ का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ-अंग्रेजी शब्द Education’ की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। विद्वानों का विचार है कि Education शब्द का संबंध लैटिन भाषा के तीन शब्दों educatium’ (एजूकेसीयम) educere’ (एजूसीयर) तथा ‘educare’ (एजूकेयर) से है। इन तीनों ही शब्दों का लैटिन भाषा में लगभग समान अर्थ है। इन शब्दों का क्रमशः अर्थ है–विकसित करना, निकालना या आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या शिक्षित करना। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक या व्यक्ति की निहित शक्तियों एवं क्षमताओं को विकसित किया जाता है या प्रस्फुटित किया जाता है। इस प्रकार का विकास जीवनभर होता रहता है; अतः शिक्षा की प्रक्रिया भी जीवनभर चलती रहती है। स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण से शिक्षा का शिय संस्थागत शिक्षा तक सीमित नहीं है।
प्रश्न 13.
शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है?
उत्तर
अनेक विद्वानों ने ‘शिक्षा’ की प्रक्रिया की व्याख्या उसके व्यापक अर्थ में की है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में एक अति व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। इस रूप में शिक्षा जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन भर निरंतर चलती रहती है। काल या अवधि के ही समान इस अर्थ के अनुसार शिक्षा प्रदान करने अथवा ग्रहण करने का क्षेत्र भी सीमित नहीं होता अर्थात् शिक्षण का क्षेत्र शिक्षा संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा जगत् ही शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा प्रदान करने का क्षेत्र है। शिक्षा की इस व्यापक व्याख्या को मैकेंजी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, “विस्तृत अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है तथा जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करता है। ये अनुभव किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि केवल विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा संस्था के अध्यापक ही शिक्षक नहीं होते बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में शिक्षक की भूमिका निभा सकता है। जिस भी व्यक्ति से कोई नई बात सीखी जाए, वही व्यक्ति उस संदर्भ में शिक्षक है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर कोई बालक भी किसी प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शिक्षक सिद्ध हो सकता है। बालक ही क्या, पर्यावरण से भी अनेक बातें सीखी जा सकती हैं। अत: पर्यावरण भी हमारे लिए शिक्षक ही है।
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से भिन्न शिक्षा के व्यापक़ अर्थ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी अति व्यापक है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, न कि विभिन्न स्तरों के प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इस तथ्य को एडलर (Adler) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, “शिक्षा मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है, यह केवल छोटे बालकों से ही संबंधित नहीं होती। यह तो जन्म से ही प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है।”
प्रश्न 14.
शिक्षा के दो कौन-से प्रमुख सामाजिक कार्य हैं? विवरण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर
शिक्षा के दो प्रमुख सामाजिक कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-
- राष्ट्रीय विकास में योगदान-राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है। वास्तव में, किसी भी राष्ट्र के संमुचित विकास के लिए आवश्यक होता है। कि उसके अधिक-से-अधिक नागरिक शिक्षित हों। अधिकांश नागरिकों के अशिक्षित होने की स्थिति में कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति नहीं कर सकता। यह दो दृष्टिकोणों से सत्य है। सर्वप्रथम तो यह सत्य है कि अशिक्षित नागरिक राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में समुचित योगदान दे ही नहीं सकते। दूसरी बात यह सत्य है कि केवल शिक्षित व्यक्ति ही इस तथ्य को समझ पाते हैं कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति का महत्त्व अधिक होता है। शिक्षा के द्वारा इस विवेक के विकास के परिणामस्वरूप राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होने लगता है।
- राष्ट्रीय एकता के विकास में योगदान–राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक उल्लेखनीय कार्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखना भी है। हमारे देश के सदंर्भ में शिक्षा का यह कार्य और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में बहुपक्षीय विविधता विद्यमान है। जातिगत, भाषागत, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधता हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक कारक है। इन कारकों के विद्यमान होने के कारण राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
प्रश्न 15.
शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? बताइए।
उत्तर
कुछ विद्वानों ने शिक्षा की प्रक्रिया में निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए इसको एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। इस मान्यता के अनुसार शिक्षा के तीन अंग हैं—शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा बालक। इस मान्यता के अनुसार शिक्षक तथा बालक के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए जॉन डीवी ने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की है। डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ-ही-साथ सामाजिक पक्ष का भी समान रूप से महत्त्व है। शिक्षा की प्रक्रिया सदैव समाज में रहकर ही चलती है। समाज से बिल्कुल अलग रहकर शिक्षा की प्रक्रिया का चल पाना संभव नहीं है। यह भी कहा जा
कता है कि समाज के सहयोग से ही बालक का मनोवैज्ञानिक विकास भी सुचारू रूप से हो सकता है। इस प्रकार, शिक्षा द्वारा बालक को सामाजिक विकास भी होता है। अतः बालक को उस समाज के लिए शिक्षित करना चाहिए, आगे चलकर जिस समाज का उसे सदस्य बनना है। यह तभी हो सकता है। जबकि बालक का शिक्षा समाज के ही माध्यम से हो। समाज द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है। कि परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में बालक को कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए तथा पढ़ाने के लिए किस-किस शिक्षण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि बालक की कार्यकुशलता में वृद्धि हो तथा वह समाज द्वारा स्वीकृत आचरण करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार बालकों को शिक्षित करता है। इसी व्याख्या के आधार पर शिक्षा के तीन अंग माने जाते हैं–शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा बालक।,
प्रश्न 16.
समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकार व्यक्तियों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं?
उत्तर
प्रांरभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकम के साथ राजनीतिक भागीदारों के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। इन अधिकारों को अधिकतर संघर्ष द्वारा प्राप्त किया जाता था। राजतंत्र की शक्तियों को सीमित करना अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत करना इसी संघर्ष का परिणाम है। फ्रीस की क्रांति तथा भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस प्रकार के आंदोलनों के उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। भारत में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार रहने की जगह चुनने का, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार, सम्मिलित हैं। राजनीतिक अधिकारों में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है तथा सार्वजनिक पद के लिए खड़ा हो सकता है। सामाजिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुचित जातियों को दिए गए विशेष अधिकार इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना भी व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार देना ही है।
अधिकार व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। समाज के बहुत-से वर्ग अन्य वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता भी इसी का ही परिणाम है। बहुत-से विकासशील देशों में सामाजिक अधिकारों को आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किए जाने लगे हैं तथा इन्हें प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया जाने लगा है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
परिवार की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
या
परिवार से आपका क्या तात्पर्य है? परिवार की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
या
परिवार से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं?
उत्तर
परिवार एक सार्वभौमिक संगठन अथवा इकाई है क्योंकि यह किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अन्य प्राणियों के समान मनुष्य में भी जाति-सृजन तथा वंश-संरक्षण की । नैसर्गिक प्रेरणाएँ होती हैं। इन प्ररेणाओं से ही परिवार तथा घर का जन्म हुआ। परिवार पति-पत्नी तथा उनकी संतान से मिलकर बनता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यह समाज की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ
परिवार-समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता-पिता, भाई-बहिन, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजी, पुत्र-पुत्री आदि होते हैं और जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं परंतु परिवार का यह रूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है। पाश्चात्य देशों में परिवार का तात्पर्य समाज की उस इकाई से लगाया जाता है जिसमें माता-पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के स्वरूप होने के कारण ही इसकी परिभाषा के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं पाया जाता है।
प्रमुख विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है–
ऑगर्बन एवं निमकॉफ (Ogbum and Nimkoff) के अनुसार-“परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवी केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है।”
बीसेंज एवं बीसेंज (Biesanz and Biesanz) के अनुसार-“एक सा अधिक बालकों सहित एक स्त्री और उनकी देखरेख करने के लिए एक पुरुष हो तो इन सबको मिलाकर एक परिवार बन जाता है।”
किंग्स्ले डेविस (Kingsley Davis) के अनुसार-“परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक-दूसरे के संबंधी होते हैं।”
मैकाइवर एंव पेज(Maclver and Page) के अनुसार-“परिवार पर्याप्त निश्चित यौन-संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने (प्रजनन) तथा लालन-पालन करने की व्यवस्था करता है।”
इलियट एवं मैरिल (Elliott and Merrill) के अनुसार–“परिवार को पति-पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनके अनुसार यह एक सामाजिक संस्था भी है और एक सामाजिक संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
बील्स एवं हॉइजर (Beals and Hoijar) के अनुसार-संक्षेप में, परिवार एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के संबंधों द्वारा बद्ध होते हैं।”
जुकरमैन (Zuckerman) के अनुसार-“एक परिवार-समूह पुरुष स्वामी, उसकी समस्त स्त्रियों और उनके बच्चों को मिलाकर बनता है। कभी-कभी एक या अधिक अविवाहित अथवा पत्नी-विहीन पुरुषों को भी सम्मिलित किया जाता है।”
बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार-“परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसमें साधारणतः माता-पिता एवं एक या अधिक बच्चे होते हैं, जिसमें स्नेह एवं उत्तरदायित्व का समान हिस्सा होता है। तथा जिसमें बच्चों का पालन-पोषण उन्हें स्वनियंत्रित एवं सामाजिक प्रेरित व्यक्ति बनाने के लिए होता है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों को एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन-पोषण को दायित्व निभाते हैं। परिवार की नींव स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों के नियोजन पर होती है। बच्चों का जन्म, लालन-पालन एवं समाजीकरण आदि इसके मुख्य कार्य होते हैं।
परिवार की प्रमुख विशेषताएँ
परिवार की कुछ मूलभूत विशेषताएँ हैं जो सामान्य रूप से विश्व के समस्त परिवारों में पाई जाती हैं। परिवार की निम्नांकित विशेषताएँ परिवार की संकल्पना को स्पष्ट करने में भी सहायक हैं-
- यौन-संबंध—यौन-संबंध की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। वास्तव में सृष्टि का अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है। मनुष्य में भी काम-भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। इस भावना की संतुष्टि के लिए ही स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के निकट आते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो स्त्री और पुरुष दोनों में पाई जाती है। सभ्य समाजों में विवाह-संबंध द्वारा इस प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है और परिवार का जन्म होता है, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि विवाह से पूर्व बनाए गए यौन-संबंधों द्वारा परिवार का जन्म नहीं होता।
- पति-पत्नी का संबंध-परिवार का विकास पति-पत्नी के यौन संबंध द्वारा होता है। बिना पति-पत्नी के संबंधों के परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। यह संबंध अनेक रूपों में हो सकता है। कुछ स्थानों पर यह संबंध एकविवाह-प्रथा के रूप में पाया जाता है तो कुछ में बहुविवाह-प्रथा के रूप में हो सकता है। स्त्री-पुरुष के संबंधों को नियमित करने वाली संस्था को ‘विवाह’ कहा जाता है।
- रक्त-संबंध-परिवार की एक अन्य विशेषता है कि उसके विभिन्न सदस्यों का एक-दूसरे से पर रक्त-संबंधों द्वारा जुड़ा होना। माता-पिता द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वह पूर्णतया उनके रक्त से संबंधित होती है। एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न समस्त संतानों में रक्त-संबंध होती है। इस रक्त-संबंध से ही परिवार का जन्म होता है। वास्तव में, रक्त-संबंध बाबा, चाचा, चाची और उनकी संतान में भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- आर्थिक सुरक्षा–प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करता है। प्रत्येक सदस्य के भोजन की व्यवस्था करना भी परिवार का कार्य हैं। परिवार में श्रम-विभाजन के नियमों का अनुसरण होता है, जिसको आधार लिंग तथा आयु है। स्त्रियाँ घर के खाने-पीने की व्यवस्था करती हैं तो पुरुष घर से बाहर अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी विशेष संपत्ति होती है जिस पर उसका अपना अधिकार होता है।
- निवास स्थान परिवार का चौथी महत्त्वपूर्ण विशेषता स्थायी निवास स्थान है। परिवार के समस्त सदस्य अपनी शारीरिक सुरक्षा तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए एक ही घर या निवास स्थान में रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर या नौकरी के लिए परिवार का कोई सदस्य किसी स्थान पर चला जाए तो इससे परिवार की समाप्ति नहीं होती; क्योंकि इस प्रकार का जाना अस्थायी होता है।
- सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान-परिवार बाल को सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी बनने का पाठ पढ़ाता है। समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार का योगदान अद्वितीय है। माता-पिता द्वारा बालक सामाजिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है तथा विभिन्न शिष्टाचारों से परिचित होता है। सामाजिकता की जो शिक्षा बालक को परिवार से प्राप्त होती है वह अन्य किसी संस्था से प्राप्त नहीं होती। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है।
- सार्वभौमिकता–परिवार एक ऐसा संघ है जो विश्व के समस्त समाजों में पाया जाता है। यदि हम अतीतकालीन इतिहास पर अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि आदिकाल से ही परिवार का अस्तित्व चला आ रहा है। इसके स्वरूप में अवश्य परिवर्तन आया है, परंतु यह सभी समाजों में आज भी पाया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि परिवार विश्व में पाई जाने वाली एक सार्वभौमिक इकाई है।
- सामाजिक सुरक्षा-परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार में विशेष स्थान या पद होता है; जैसे माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहिन इत्यादि। परिवार के सदस्य अपनी ही नहीं, अपितु परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अपमान तथा दिवालिएपन आदि की नौबत न आ सके।
- भावात्मक आधार-परिवार की अन्य विशेषता उसका भावात्मक आधार है। यह मनुष्य की अनेक स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर आधारित होता है; जैसे-वात्सल्य, प्रेम, यौन सम्बन्ध, दया तथा ममता आदि। अन्य संस्थानों या संघों में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ नहीं पाई जातीं।
- स्थायी और अस्थायी प्रकृति-परिवार एक स्थायी संगठन भी है और अस्थायी भी। परिवार का निर्माण पति-पत्नी से होता है, परंतु यदि इनमें से किसी एक की मुत्यु हो जाती या तलाक हो जाता है तो परिवार भंग हो जाती है। इस पर भी संस्था के रूप में परिवार का स्वरूप स्थायी होता है क्योंकि एक परिवार के भंग हो जाने से परिवार नामक संस्था भंग नहीं हो जाती।
- सीमित आकार-परिवार प्राणिशास्त्रीय दशाओं पर आधारित होता है। परिवार का सदस्य वही व्यक्ति बन पाता है जो कि उसमें जन्म लेता है। व्यक्ति विवाह द्वारा उसका सदस्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। इन कारणों से परिवार का आकार सीमित होता है।
परिवार के भेद या प्रकार
परिवार का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। यहाँ हम तीन प्रकार के प्रमुख वर्गीकरणों का ही उल्लेख करेंगे-
(अ) सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण
सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
- पितृमूलक परिवार-इस प्रकार के परिवार में सबसे अधिक आयु का पुरुष परिवार का प्रधान होता है। वह प्रधान पुरुष (कर्ता) ही परिवार की देखभाल करता है तथा अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार के परिवार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। वंश पिता (प्रधान) के नाम पर चलता है तथा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। पितृमूलक परिवार पितृसत्तात्मक होने के साथ-साथ पितृस्थानीय भी होते हैं अर्थात् वधू विवाह के पश्चात् अपने पति के घर रहती है। हमारे देश में अधिकांश परिवार पितृमूलक एवं पितृसत्तात्मक ही है।
- मातृमूलक परिवार–मातृमूलक परिवार में माता परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंत्रण में शेष सदस्य रहते हैं। इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्त्व होता है। वंश का नाम भी पत्नी अर्थात् स्त्री के नाम से चलता है। मातृमूलक परिवारों का चलन अब बहुत कम है। भारत में मालाबारे और असम में ही मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार मातृस्थानीय भी होते हैं अर्थात् विवाह के पश्चात् लड़का-लड़की वालों के घर रहने लगता है।
(ब) विवाह-प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण
विवाह-प्रणाली के आधार पर परिवार को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
- एकविवाही परिवार–इस प्रकार के परिवार में पति केवल एक ही विवाह करता है। आजकल इस प्रकार के परिवारों का ही अधिक प्रचलन है। ईसाइयों और यहूदियों में अतीतकाल से ही इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
- बहुपत्नी परिवार—जिस परिवार का पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रखता है वह बहुपत्नी परिवार कहलाता है। बहुविवाह का प्रचलन अनेक देशों में पाया जाता था। संपन्न लोग अपनी वासनों की पूर्ति के लिए तथा कई बार प्रतिष्ठा के रूप में एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे। भारत के जमींदार, सामन्त तथा राजा-महाराजा इसके उदाहरण रहे हैं। इसके अलावा जब समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियाँ रखने पर मजबूर होता है, परंतु अब यह प्रथा हानिकारक होने के कारण धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।
- बहुपति परिवार इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। हमारे देश में टोडा और खस जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। चकराता में निवास करने वाली खस जनजाति में सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है।
(स) संगठन के आधार पर वर्गीकरण
पारिवारिक संगठन या संरचना के आधार पर परिवार को अग्रलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकती है
- एकाकी परिवार-एकाकी परिवार में केवल पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के परिवार प्रायः पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं। भारत में भी नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
- संयुक्त परिवार-संयुक्त परिवार एकाकी परिवार से आकार में बड़ा होता है। इस प्रकार के परिवार में पति-पत्नी, माता-पिता, चाचा-चाची, बेटे-बहू तथा पौत्र-प्रपौत्र आदि रहते हैं। परिवार का प्रधान (कर्ता) सबसे अधिक वृद्ध पुरुष होता है और उसी के द्वारा परिवार का संचालन होता है। हमारे देश में प्राचीनकाल में ही इस प्रकार के परिवारों के पाए जाने की उल्लेख मिलता है तथा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
![]()
प्रश्न 2.
परिवार के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।
या
परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर
परिवार के कार्य अथवा महत्त्व सामाजिकता का प्रथम पाठ मनुष्य परिवार में ही पढ़ता है; अत: सबसे पहली सामाजिक संस्था परिवार ही है, जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाती है। संक्षेप में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार का महत्त्व इसके द्वारा निष्पादित निम्नलिखित कार्यों से आँका जा सकता है-
(1) प्राणिशास्त्रीय कार्य
परिवार के प्राणिशास्त्रीय कार्य निम्नलिखित हैं-
- यौन-इच्छा की पूर्ति-परिवार का प्रथम कार्य स्त्री-पुरुष की यौन इच्छा की पूर्ति करना है। यह सत्य है कि व्यक्ति परिवार के बाहर भी अपनी काम-इच्छा की पूर्ति कर सकता है, परंतु उसका यह कृत्य पूर्णतया असामाजिक माना जाता है। विवाह के द्वारा ही समाज स्त्री-पुरुष के यौन-संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।
- सन्तानोत्पत्ति-संतान की कामना करना प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए स्वाभाविक है। परिवार मनुष्य की इस जन्मजात इच्छा को पूरा करता है। पति-पत्नी के यौन-संबंधों की स्थापना के पश्चात् संतान की उत्पत्ति होती है। विवाह तथा परिवार की संस्थाओं के दायरे में उत्पन्न हुई। संतान को वैध सन्तान माना जाता है।
- संतान का लालन-पालन-जन्म के समय शिशु पूर्णतया अबोध होता है। उसके लालन-पालन और भरण-पोषण का कार्य परिवार द्वारा ही होता है। यदि परिवार द्वारा बालक की उपेक्षा की जाए, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। परिवार का कार्य केवल प्रजनन अथवा संतानोपत्ति ही नहीं है, अपितु संतान का लालन-पालन भी है।
- भोजन की व्यवस्था परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, जो सभी की एक मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। सदस्यों में पाया जाने वाला प्रारम्भिक सहयोग इसमें सहायता प्रदान करता है।
- जीवन की सुरक्षा-परिवार के सदस्य परस्पर मिलकर रहते हैं और एक-दूसरे की सुरक्षा तथा रोग-निवारण में योगदान प्रदान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार में अपने को हर प्रकार से सुरक्षित अनुभव करता है। यह एक प्रकार से सदस्य के लिए सामाजिक बीमा है।
- वस्त्रों की व्यवस्था–परिवार अपने सदस्यों के लिए वस्त्रों की भी व्यवस्था करता है। यह भी एक मौलिक व आधारभूत आवश्यकता है।
- निवास की व्यवस्था परिवार के सदस्य भली प्रकार सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए परिवार निवास स्थान या घर की भी व्यवस्था करता है।
(2) सामाजिक कार्य
परिवार के अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य हैं। इसके प्रमुख सामाजिक कार्य निम्नांकित हैं-
- बालक का समाजीकरण—परिवार का प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य बालक का सामाजीकरण करना है। जन्म लेने के पश्चात बालक में अनेक पाशविक प्रवृत्तियाँ होती हैं। परिवार के वातावरण द्वारा ही इन प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गन्तीकरण होता है, जिससे वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। अन्य लोगों से व्यवहार करना, उठने-बैठने तथा बात करने का शिष्टाचार आदि बालक परिवार से ही सीखता है। बाल्यावस्था में ही नहीं, बल्कि जीवन भर परिवार किसी-न-किसी रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान प्रदान करता है।
- सामाजिक विरासत का हस्तांतरण व प्रसार करना–परिवार सामाजिक विरासत को प्रसार एवं हस्तांतरण करता है। यह जनरीतियाँ, कानून, विश्वास, रूढ़ियाँ, नैतिक नियम, शिक्षा आदि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान करता है तथा उनका संग्रह और विस्तार करता है।
- सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना–परिवार की स्थिति के अनुसार उसके सदस्यों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि उसके सदस्यों को किन-लोगों में उठना-बैठना चाहिए। वैवाहिक संबंधों की स्थापना भी इसी आधार पर की जाती है।
- सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना-परिवार अपने सदस्यों के सामाजिक अपमान दिवालिएपन आदि से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। परिवार ही एक ऐसा संगठन है। जो व्यक्ति के सामाजिक सम्मान की सुरक्षा के प्रति चिंतित रहता है तथा उसे यथासंभव सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- जीवनसाथी के चुनाव में सहायक–परिवार अपने सदस्यों के विवाह या जीवनसाथी के चुनाव . में योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार परिवार एक अन्य परिवार को जन्म देता है।
- सामाजिक नियंत्रण में सहायक–परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण तथा प्रबल अभिकरण है। परिवार अपने सभी सदस्यों के व्यवहारों को निरंतर रूप से नियंत्रित करता रहता है तथा व्यक्ति के असामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। परिवार द्वारा लागू किया गया नियंत्रण अनौपचारिक तथा अधिक प्रभावशाली होता है।
(3) मनोवैज्ञानिक कार्य
परिवार द्वारा अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्य भी किए जाते हैं। इनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
- परिवार बालकों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- परिवार बालकों का संवेगात्मक विकास उचित दिशा में करता है।
- परिवार में अनेक मूलप्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है। काम, वात्सल्य, सहानुभूति तथा प्रेम इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- अनेक मानसिक प्रक्रियाएँ; जैसे-जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, विचार आदि का विकास परिवार में ही होता है।
(4) धार्मिक कार्य
परिवार वह स्थल है जहाँ अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक बातों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। परिवार के समस्त सदस्य सामान्य रीति से ईश्वर की उपासना करते हैं। छोटे-छोटे बालक अपने माता-पिता से कहानियाँ सुनकर ईश्वर और अध्यात्मक संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। माता-पिता के धार्मिक आचरण बालकों को प्रभावित करते हैं और वे अनुकरण द्वारा अनेक धार्मिक क्रियाएँ सीख जाते हैं। परिवार में आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सवों द्वारा भी बालकों को धर्म को ज्ञान प्राप्त होता है।
(5) आर्थिक कार्य
परिवार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आर्थिक कार्य निम्नांकित हैं-
- श्रम-विभाजन-परिवार के अधिकांश कार्य श्रम-विभाजन पर आधारित रहते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता और क्षमता तथा लिंग और आयु के आधार पर अपना-अपना कार्य करता है। पिता द्वारा प्रायः धनोपार्जन होता है तो माता घर में खाने-पीने तथा सफाई आदि की प्रबंध करती है। पुत्र साग-सब्जी तथा सौदा आदि लाते हैं तो बेटियाँ अपनी माँ के घरेलू कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर परिवार के सभी कार्य सुविधापूर्वक हो जाते हैं वहीं साथ-ही-साथ प्रत्येक व्यक्ति को पारस्परिक कार्यों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण–पविावर में बालक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। पिता यदि दुकानदान, लुहार या बढ़ई है तो बालक बचपन से ही उसके साथ रहकर उसके व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परिवार व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
- उत्पादन की प्रेरणा-परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक उत्पादन की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य परिवार की देशी को सुधारने हेतु कुछ-न-कुछ आर्थिक उत्पादन की चेष्टा करता है।
- आर्थिक क्रियाओं का केंद्र–अतीतकाल से ही परिवार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ परिवार से ही हुआ और वहीं से उनका प्रसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ।
- उत्तराधिकार का निश्चय–परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार का भी निश्चय होता है। गृह-विभाजन किस प्रकार का हो, इसका निश्चय परिवार में ही होता है।
(6) शैक्षिक कार्य
परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा गया है। आगस्त कॉम्टे के शब्दों में, “परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है।” पेस्तोलॉजी के अनुसार, “परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। वास्तव में, परिवार में बालक अपने माता-पिता तथा बड़ों का अनुकरण करके अनेक बातें सीखता है तथा अपना बौद्धिक विकास करता है। प्राचीन समाजों में शिक्षा संस्थाओं का कार्य भी परिवार ही करते हैं तथा आज भी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में परिवार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
(7) सांस्कृतिक कार्य
परिवार का संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परिवार में रहकर बालक अपनी संस्कृति से परिचित होता है। परिवार का सांस्कृतिक वातावरण बालक को समाज की संस्कृति का ज्ञान कराता है। बालक अनुसरण द्वारा भाषा और अन्य संस्कृति संबंधी बातें सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन का अंग बनाते हैं। रीति-रिवाज, परंपराओं तथा रीतियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ परिवार बालकों को उनका ज्ञान भी कराता है। परिवार ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
(8) राजनीतिक कार्य
परिवार एक प्रशासकीय इकाई भी है। अन्य शब्दों, यदि परिवार को राज्य का छोटा रूप कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। भूमि, जनसंख्या, सरकार आदि राज्य के आवश्यक तत्त्व परिवार में उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार राज्य में प्रभुत्त्व सर्वोच्च होता है उसी प्रकार परिवार में प्रधान (कर्ता) को प्रभुत्व सर्वोच्च होता है। उसकी आजा का पालन प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। परिवार की पंरपराओं और नियमों का पालन प्रत्येक सदस्य उसी प्रकार करता है जिस प्रकार राज्य के कानूनों का पालन प्रत्येक नागरिक करता है। सिडनी ई० गोल्डस्टीन (Sydme E. Goldstein) के शब्दों में, “परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशुगृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का विकास होता है।’
(9) मनोरंजनात्मक कार्य
मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का भी अपना अलग महत्त्व है। मनुष्य के लिए दिन भर परिश्रम करने के पश्चात मनोरंजन करना आवश्यक हो जाता है। मनोरंजन से शरीर की थकावट दूर होती है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है। परिवार स्वस्थ मनोरंजन का प्रमुख केंद्र रहा है। थका हुआ व्यक्ति घर में अपने बाल-बच्चों के बीच बैठकर आनंद और स्फूर्ति का अनुभव करता है। छोटे बालक अपने दादा तथा दादी से कहानियाँ आदि सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। देवर-भाभी तथा ननद-भाभी के कुछ रिश्ते बहुत मधुर होते हैं तथा परिवार में रहकर इन रिश्तों वाले सदस्य भरपूर आनंद उठाते हैं।
(10) नागरिकता का प्रशिक्षण स्थल
मैजिनी के अनुसार, “बालक नागरिकता का फ्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के मध्य सीखता है। परिवार बालक में अनेक नागरिकता के गुणों का विकास करता है। इस संबंध में परिवार के प्रमुख कार्य अग्रांकित हैं-
- स्नेह की शिक्षा–स्नेह की शिक्षा बालक सर्वप्रथम माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। टी० रेमण्ड का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि “घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। माता-पिता का स्नेह बालक में भी प्रेम के बीज डाल देता है। बालक भी अपने माता-पिता से प्रेम करना सीख जाता है। भविष्य में यही पारिवारिक प्रेम व्यापक होकर सामाजिक प्रेम में परिणत हो जाता है।”
- सहानुभूति की शिक्षा-परिवार में माता-पिता बालक के दु:ख को देखकर तुरंत चिंतित हो उठते हैं और दौड़-भाग कर उनके दु:ख को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी सच्ची सहानुभूति का प्रदर्शन बालक पर अत्यन्त गहरा प्रभाव डालता है और वह भी समय अनुसार परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है।
- निःस्वार्थता की शिक्षा–माता-पिता अपने बालक से नि:स्वार्थ प्रेम करते हैं और माता-पिता उनका लालन-पालन किसी स्वार्थ की भावना से नहीं करते। इससे परिवार के सदस्यों में नि:स्वार्थता के गुण का विकास होता है।
- सहयोग की शिक्षा-सामाजिक जीवन में सहयोग का विशेष महत्त्व है। सामाजिक जीवन का आधार सहयोग ही है। बालक सहयोग का प्रथम पाठ परिवार में ही पढ़ता है; क्योंकि वह देखता है कि परिवार के समस्त सदस्य मिलजुलकर घर का कार्य करते हैं। विद्वान बोसो के अनुसार, परिवार वह स्थान है, जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का या नया पाठ सीखती है कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता।”
- कर्तव्यपालन और आज्ञापालने की शिक्षा–आज्ञापालन और कर्तव्यपालन की शिक्षा भी बालक परिवार में ही सीखता है। प्रत्येक बालक अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझता है। इस प्रकार वह अनुशासन का पाठ सीखता है।। निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। परिवारों का वर्गीकरण विविध आधारों पर किया गया है। परिवार प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं को पूरा करके तथा अन्य सभी कार्यों के कारण समाजीकरण का एक प्रमुख अभिकरण माना जाता है। परिवार को इसीलिए बच्चे की प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है।
![]()
प्रश्न 3.
विवाह का क्या अर्थ है? विवाह के प्रमुख उद्देश्यों एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए।
या
विवाह को परिभाषित कीजिए। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में बताइए।
उत्तर
मानव समाज में विवाह एक प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण संस्था है जो कि सार्वभौमिक है; अर्थात् सभी समाजों में किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है। हिंदू समाज में तो इसे विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम में विवाह द्वारा प्रवेश करना एक अनिवार्य कर्म ठहराया गया है। प्रायः विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री तथा पुरुष के यौन-संबंधों को नियंत्रित तथा नियमित करना माना जाता है। परंतु हिंदू धर्म के अनुसार, विवाह के एक नहीं वरन् अनेक उद्देश्य है, जिनमें धर्म तथा प्रजा (संतान) अनिवार्य हैं और यौन-संबंधों की संतुष्टि अंतिम उद्देश्य है।
विवाह का अर्थ एवं परिभाषाएँ
विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संस्था है, जिसमें स्त्री-पुरुष को काम-वासना की संतुष्टि के लिए समाज द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है। समाज की यह स्वीकृति कुछ संस्कारों को पूरा करने के पश्चात् ही प्राप्त होती है। इस अर्थ में विवाह यौन-संबंधों के नियंत्रण एवं नियमन का साधन है। अन्य शब्दों में, समाज द्वारा अनुमोदित स्त्री-पुरुष के संयोग को विवाह कहते हैं। विभिन्न समाजाशास्त्रियों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है-
- जेम्स (James) के अनुसार-“विवाह मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली संस्था है जो कि यौन-संबंध, गृह-संबंध, प्रेम तथा मानवीय स्तर पर व्यक्तित्व के जैविकीय, मनोवैज्ञानिक सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है।”
- जेकब्स एवं स्टर्न (Jacobs and Stern) के अनुसार–“विवाह एक अथवा अनेक पति तथा पत्नियों के सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह उस संस्कार का भी नाम है, जिसके द्वारा पति-पत्नी आपस में सामाजिक संबंधों में बँधे होते हैं।”
- वेस्टरमार्क (Westermarck) के अनुसार-“विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक अथवा अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है, जो प्रथा व कानून द्वारा स्वीकृत होता है और जिसमें संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है।”
- बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार-“विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है।”
- मैलिनोव्स्की (Malinowski) के अनुसार–‘विवाह केवल यौन-संबंधों को अपनाना नहीं है, अपितु यह सामाजिक संस्था है, जो मिश्रित सामाजिक परिस्थितियों पर आश्रित है।”
- गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin)के अनुसार-“विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना का समाज-स्वीकृत तरीका है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है, जिसके अंतर्गत स्त्री-पुरुष समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से आपस में पति-पत्नी के रूप में यौन-संबंध स्थापित करके स जान को जन्म देते हैं तथा उनका समुचित पालन-पोषण करते हैं।
विवाह के प्रमुख उद्देश्य
विवाह के कुछ सर्वमान्य उद्देश्य हैं जो कि इस संस्था द्वारा समाज में पूरे किए जाते हैं। विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- यौन-सुख की प्राप्ति-प्रायः विवाह का उद्देश्य यौन-सुख प्राप्त करना माना जाता है। विवाह व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी यौन-इच्छा की तृप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। विवाह संस्था के अंतर्गत स्थापित हुए यौन-संबंधों को ही समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।
- संतानोत्पत्ति तथा बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना—विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। विवाह द्वारा उत्पन्न संतान ही उसके वंश को चलाती है। विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई संतान को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है।
- परिवार का निर्माण करना—विवाह केवल यौन-इच्छा की संतुष्टि का साधन-मात्र ही नहीं है, अपितु इससे स्त्री और पुरुष पत्नी एवं पति के रूप में परिवार का निर्माण करते हैं। वास्तव में विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य परिवार का निर्माण करना ही है।।
- मनोवैज्ञानिक उद्देश्य–विवाह का उद्देश्य स्त्री-पुरुष को मानसिक संतोष प्रदान करना भी है। मानसिक संतोष के कारण ही परिवार का सदस्य बड़े-से-बड़ा दु:ख सहन करने को तैयार रहते हैं।
- आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य–कुछ विद्वानों के अनुसार विवाह का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। स्त्री-पुरुष विवाह द्वारा गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा गृहस्थी चलाने हेतु आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी परस्पर सहयोग देते हैं। यह उद्देश्य अन्य उद्देश्यों की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण है।
- संबंधों में स्थायित्व-विवाह का एक अन्य उद्देश्य स्त्री-पुरुष संबंधों में स्थायित्व लाना है। क्योंकि विवाह संस्था समाज द्वारा स्वीकृत होती है, इसलिए यह समाज में स्थायी संबंधों की स्थापना और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है।
विवाह के प्रमुख स्वरूप या प्रकार
विवाह एक अत्यंत प्राचीन संस्था है। मानव समाज में इसके अनेक रूप मिलते हैं जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-
1. एकविवाह-एकविवाह से तात्पर्य उस विवाह से है, जिसमें एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करें तथा इसी प्रकार एक स्त्री केवल एक ही पुरुष से विवाह करे। इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है; क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो सकती है, जिस पर उसका यौन-संबंधों के बारे में पूर्ण अधिकार होता है। केवल पत्नी की मुत्यु के पश्चात् पति तथा पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है। तलाक के पश्चात् भी दूसरा विवाह किया जा सकता है। सभी सभ्य समाजों में एकविवाह प्रथा का ही प्रचलन है। वेस्टरमार्क तथा मैलिनोव्स्की जैसे विद्वानों ने एकविवाह को ही विवाह का सच्चा व आदि स्वरूप माना है।।
2.बहुविवाह-बहुविवाह वह विवाह है, जिसमें कई पुरुष एक स्त्री से या कई स्त्रियाँ एक पुरुष से विवाह करती हैं। यदि जीवनसाथी की संख्या एक से अधिक है तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। बहुविवाह के निम्नलिखित दो रूप होते हैं|
- बहुपत्नी विवाह-इस विवाह में एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन मुख्यतया धनी वर्ग, मुसलमानों तथा कुछ जनजातियों में पाया जाता है, परंतु अब इस प्रकार के विवाह का प्रचलन कम होता जा रहा है। इस प्रकार के विवाह के अनेक कारण है; जैसे—प्रथम पत्नी से संतान का न होना, किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होना, स्त्रियों की स्थिति निम्न होना, सामाजिक मान्यताओं द्वारा स्वीकृत तथा कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी अनेक पत्नियाँ रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुरुषों का अधिक कामुक प्रवृत्ति का होना भी बहुपत्नी विवाह का एक कारण है।
- बहुपति विवाह-इसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। बहुपति प्रथा का प्रचलन सभ्य समाज में नहीं है। कुछ जनजातियों (जैसे खस इत्यादि) में इस तरह का विवाह पाया जाता है। इस प्रकार के विवाह के कारण भी अनेक होते हैं; जैसे—प्रथम, जब किसी समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या
अधिक होती है। दूसरे, कहीं-कहीं आर्थिक कारणों तथा निर्धनता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक् रूप से परिवार बसाना संभव नहीं होता, इसलिए अनेक पुरुष मिलकर एक परिवार बसाते हैं जैसा कि लद्दाख में होता है। तीसरे, जब वधू-मूल्य अधिक होता है, तब भी इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। बहुपति विवाह भी दो प्रकार के हो सकते हैं—प्रथम प्रकार हैं भ्रातृक बहुपति विवाह तथा द्वितीय है अभ्रातृक बहुपति बिवाह। प्रथम प्रकार के विवाह में एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं।
तथा द्वितीय प्रकार में ये पति कोई अन्य भी हो सकते हैं।
3. समूह विवाह-उविकासवादियों के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में समूह विवाहों का प्रचलन था जैसा कि इस विवाह के नाम से ही स्पष्ट है; इसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है। यह विवाह समूह के किसी पुरुष विशेष एवं स्त्री विशेष में न होकर दो संपूर्ण समूहों के स्तर पर होता है। इसमें प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री से यौन-संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होता है। समूह विवाह जनजातियों में पाया जाता था तथा यह विवाह के प्रारंभिक रूप का द्योतक माना गया है। ली तथा ली (Lee and Lee) के अनुसार समूह विवाह से तात्पर्य उस विवाह से हैं, जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक पुरुष दो तथा दो से अधिक स्त्रियाँ परस्पर विवाह करते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार तिब्बत, भारत व लंका में यह विवाह पाया जाता था। विवाह के इस प्रकार का उल्लेख ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में भी मिलता है, जहाँ एक कुल की सभी लड़कियाँ दूसरे कुल की भावी पत्नियाँ समझी जाती हैं।
कुछ विद्वानों ने समूह विवाह को साम्यवाद एवं समानतावाद का द्योतक माना है, परंतु इस प्रकार के विवाह वस्तुतः विवाह के वास्तविक अर्थ से ही मेल नहीं खाते हैं। इसके परिणामस्वरूप समूहों में अस्थायित्व एवं संघर्ष की भावना विकसित होती है। यद्यपि उविकासवादी इसकी कल्पना विवाह एवं परिवार के प्रारंभिक रूप में करते हैं, तथापि आजकल इस प्रकार के विवाह अशोभनीय माने जाते हैं। शायद इसलिए विश्व में अब इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं।
प्रश्न 4.
हिंदू विवाह के परंपरागत निषेध कौन-कौन से हैं? इन निषेधों में आजकल सर्वाधिक प्रभावी निषेध कौन-सा है? स्पष्ट रूप से समझाइए।
या
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की विवेचना कीजिए।
या
अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह नियमों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
प्रत्येक समाज विवाह के संबंध में कुछ नियमों का पालन करता है। ये नियम दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, वे नियम जो यह तय करते हैं कि विवाह कहाँ किया जाए तथा दूसरे, वे नियम जो यह बताते हैं कि विवाह कहाँ नहीं किया जाए। हिंदू समाज में भी इस प्रकार के नियमों का पालन होता है; जिन्हें ‘हिंदू विवाह के निषेध’ कहा जाता है।
हिंदू विवाह के प्रमुख निषेध
हिंदू विवाहों में पाए जाने वाले निषेध चार प्रकार के हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित हैं-
(अ) अनुलोम अथवा कुलीन विवाह
अनुलोम या कुलीन विवाह उस विवाह को कहते हैं, जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है। रिजले के अनुसार, “क्योंकि आर्यों में स्त्रियों की कमी थी अतः उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की कन्याओं से विवाह किया, परंतु अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अपनी कन्याएँ मूल निवासियों को नहीं दीं।” ‘महाभारत’ में लिखा है कि “ब्राह्मण तीन वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्या से, क्षत्रिय दो वर्ण अर्थात् क्षत्रिय तथा वैश्य की कन्या से और वैश्य अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करे तो उत्तम संतान उत्पन्न होती है। यह विवाह शास्त्रों के अनुसार ही मान्य रहा है। इस प्रकार के विवाहों ने बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च वर्ग के लोग एक से अधिक पत्नियाँ रखने लगे। उच्च वर्ण के लड़कों की माँग बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिला। इसने स्त्रियों के स्तर को निम्न कर दिया। अनुलोम विवाहों ने संतानों की समस्याओं को भी जन्म दिया। विषम जाति के माता-पिता से
उत्पन्न बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा।
(ब) प्रतिलोम विवाह
प्रतिलोम विवाह एक प्रकार से अनुलोम विवाह का विपरीत होता है। यह विवाह हिंदू विवाह संबंधी वह नियम है जिसकी सहायता से निम्न वर्ण अथवा कुल के लड़के का विवाह उसमें उच्च वर्ण अथवा उच्च कुल की लड़की के साथ होना अवैध और निंदनीय समझा गया है अथवा समझा जाता है। स्मृतिकार प्रतिलोम विवाहों का उग्रता के साथ विरोध करते हैं। ब्राह्मण कन्या का शूद्र पुरुष के साथ विवाह विशेष रूप से निषिद्ध बताया गया है। यदि कोई शूद्र, ब्राह्मण कन्या से संबंध स्थापित कर लेता है तो स्मृतिकारों के अनुसार उसे सार्वजनिक स्थान पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। वर्तमान युग में इस प्रकार के बंधन समाप्त हो गए हैं।
यद्यपि प्राचीनकाल में केवल अनुलोम विवाह को ही मान्यता प्राप्त थी, प्रतिलोम विवाह को नहीं, परंतु समकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की महत्ता कम होने के कारण इन दोनों प्रकार के विवाहों की महत्ता कम हो गई है। आज अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता प्राप्त होती जा रही है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक भी है।
(स) अंतर्विवाह
अंतर्विवाह का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह, वर्ण या जाति के अंदर ही विवाह करना। प्राचीनकाल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था अतः लोग सामान्यतया अपने वर्ण में ही विवाह करते थे, परंतु धीरे-धीरे अनेक जातियों का विकास हो गया और लोग अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करने लगे। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में गौड़ ब्राह्मण केवल गौड़ ब्राह्मणों में ही विवाह करते हैं। इस प्रकार अंतर्विवाह एक ऐसी वैवाहिक मान्यता है जिसमें एक स्त्री अथवा पुरुष को अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करने का नियम होता है। अन्य शब्दों में, हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर विवाह करने का निषेध है। इसी निषेध के पालन के लिए अंतर्विवाही समूहों का निर्माण किया गया। जाति प्रथा की परिभाषा के अनुसार, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। इस प्रकार के निषेधों का प्रमुख कारण प्रजातीय शुद्धता, रक्त की शुद्धता तथा जातीय संगठन को दृढ़ बनाने की इच्छा प्रमुख रहे हैं।
यद्यपि आज अधिकांशतया अंतर्विवाही मान्यताओं का पालन तो किया जाता है, तथापि अंतर्जातीय विवाहों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–
- सह-शिक्षा के प्रसार एवं युवक-युवतियों के पारस्परिक संपर्क ने विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है।
- शिक्षा के प्रसार ने जनसाधारण को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कर दिया है।
- औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण दृष्टिकोण के व्यापक होने का परिणाम।
- दैहेज प्रथा के दोषों के कारण।
- व्यावसायिक कार्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्त्री-पुरुषों का साथ-साथ काम करना।
- यातायात के साधनों के विकास का कारण।
- युवक व युवतियों में स्वयं जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्र प्रवृत्ति।।
- विभिन्न सामाजिक सुधारों के प्रभाव।
(द) बहिर्विवाह
बहिर्विवाह का तात्पर्य है, अपने रक्त-समूह आदि के अंतर्गत आने वाले सदस्य से विवाह न करना। इस मान्यता के अनुसार विवाह अपने प्रवर, गोत्र और सपिंड वाले परिवारों में नहीं किया जा सकता। हिंदुओं में तीन प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन है-
1. प्रवर बहिर्विवाह-‘प्रवर’ शब्द का अर्थ है आह्वान करना। वैदिक काल में पुरोहित जिस समय अग्नि प्रज्वलित करते थे, उस समर्म-अपने ऋषि-पूर्वजों को नाम लेते थे। आगे चलकर एक ऋषि का आह्वान करके यज्ञ करने वाले व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे को संबंधी समझने लगे। यह सत्य है कि ये संबंध धार्मिक भावना पर आधारित थे, पंरतु इस पर भी वे अपने को एक वंश का सदस्य समझने लगे। ये सभी सदस्य प्रवर माने जाने लगे और उनमें आपस में विवाह संबंध
का निषेध हो गया।
2. गोत्र बहिर्विवाह-गोत्र बहिर्विवाह को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि ‘गोत्र के अर्थ को समझा जाए। मजूमदार व मदन के शब्दों में, “एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंश-समूहों का योग होता है, जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं। यह पूर्वज मनुष्य, मनुष्य के समान पशु, पेड़, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है। गोत्र के संबंध में यह प्रथा प्रचलित है कि एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच में निकट रक्त-संबंध होते हैं। इसलिए एक ही गोत्र के सभी युवक-युवतियाँ एक-दूसरे के भाई-बहन हैं। अतः सगोत्र अथवा अंत:गोत्र विवाहों पर प्रतिबन्ध है; क्योंकि हिंदू समाज में भाई-बहन के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं।
हो सकते।।
3. सपिंड बहिर्विवाह-पिंड का अर्थ रक्त-संबंध से है। हिंदू समाज में सपिंड’ में वैवाहिक संबंध का निषेध किया गया है। सपिंड का संबंध माता की ओर से पाँच पीढ़ियों तक और पिता की ओर से सात पीढ़ियों तक माना जाता है। विज्ञानेश्वर ने सपिंड की व्याख्या इस प्रकार की है, एक ही पिंड अर्थात् एक देह से संबंध रखने वालों में शरीर के अवयव समान रहने के कारण सपिंड संबंध होता है। पिता और पुत्र सपिंड है। इसी प्रकार दादा आदि के शरीर के अवयव पिता द्वारा पोते में आने से पुत्री की माता के साथ सपिंडता होती है; अतः जहाँ-जहाँ ‘सपिंड शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ एक शरीर के अवयवों का संबंध समझना चाहिए। इस प्रकार, पिता से सात और माता से पाँच पीढ़ी के बीच लड़के और लड़कियों में विवाह नहीं हो सकता।
प्रश्न 5.
नातेदारी व्यवस्था क्या है? नातेदारों के भेद तथा नातेदारी शब्दावली को स्पष्ट कीजिए।
या
नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न रीतियों एवं श्रेणियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर
साधारण शब्दों में नातेदारी व्यवस्था रिश्ते-नाते के आधार पर बने मानवीय संबंधों की एक व्यवस्था है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के सूत्र होते हैं जो या तो वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों या विवाह के माध्यम से संबंधियों को जोड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति दो परिवारों का सदस्य माना जाता है—प्रथम, उस परिवार का जिसमें उसका जन्म हुआ है तथा द्वितीय, उस परिवार का जिसमें उसका विवाह हुआ है। रक्त के माध्यम से नातेदारों को समरक्त नातेदार तथा विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है।
नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषाएँ
मानव का जन्म परिवार में होता है। यहीं से उसका पालन-पोषण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति परिवार से निरंतर कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है। परिवार में ही उसे अपने रीति-रिवाजों, परंपराओं एवं रूढ़ियों की शिक्षा मिलती है। परिवार के सदस्य ही मानव के विचारों, मूल्यों, जीवन के ढंगों, भावनाओं आदि को विकसित करते हैं। प्रत्येक बालक को माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, दादा-दादी, मामा-मामी अनेक प्रकार के रिश्तेदारों का पता परिवार से ही चलता है। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारी की ही व्यवस्था है। इसे अग्र प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है-
- चार्ल्स विनिक (Charles Winick) के अनुसार-“नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं।”
- रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के अनुसार “नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है।”
नातेदारी के भेद
नातेदारी को संबंधों के आधार पर निम्नलिखित दो भेदों में विभाजित किया जा सकता है-
- विवाह संबंधी नातेदारी।।
- रक्त संबंधी नातेदारी तथा
इन दोनों प्रकारों में निम्न प्रकार के नातेदार सम्मिलित किए जाते हैं-
- विवाह संबंधी नातेदारी—इसमें हम उन सब नातेदारों को सम्मिलित करते हैं जो विवाह के संबंध के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ–एक स्त्री अपने पति अथवा एक पति का अपनी पत्नी से संबंध अथवा पति-पत्नी, बहनाई, दामाद, जीजा, फूफां, नन्दोई, मौसा, साढ़, पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि रिश्तेदारों को विवाह संबंधी नातेदारों में सम्मिलित किया जा सकता है।
- रक्त संबंधी नातेदारी- इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो समान रक्त के संबंध के आधार पर एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ-भाई-बहन, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी इत्यादि को इस श्रेणी में रखा जाता है।
नातेदारी शब्दावली
प्रत्येक समाज में नातेदारों को भिन्न-भिन्न शब्दों का संबोधन करके बुलाया जाता है। मॉर्गन के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार की नातेदारी शब्दावलियों का अधिक प्रचलन है-
- विशिष्ट नातेदारी शब्दावली—इसमें प्रत्येक संबंधी के लिए एक पृथक् शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ, चाचा, मामा, मौसा इत्यादि इस शब्दावली केप्रमुख उदाहरण हैं। इस शब्दावली के अनुसार एक नातेदार के लिए प्रयुक्त शब्द का प्रयोग किसी अन्य नातेदार के लिए नहीं किया जा सकता है।
- वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली–इसमें अनेक नातेदारों को एक ही श्रेणी में रख दिया जाता है। और सबको एक ही नाम से संबंधित किया जाता है। उदाहरणार्थ-अंग्रेजी के शब्द ‘अंकल का प्रयोग चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा आदि संबंधियों के लिए किया जाता है, जबकि कजिन शब्द का प्रयोग चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई-बहनों के लिए किया जाता है।
नातेदारी की श्रेणियाँ
- प्राथमिक नातेदार-जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा प्रत्यक्ष वैवाहिक यो रक्त संबंध होता है, उन्हें हम प्राथमिक नातेदार कहते हैं। प्राथमिक नातेदारों में आठ संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। ये हैं—पति-पत्नी, पिता-पुत्र, मामा-पुत्री, माता-पुत्र, छोटे-बड़े भाई, छोटी-बड़ी बहन तथा भाई-बहन। ये वे प्रत्यक्ष संबंधी हैं जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है।
- द्वितीयक नातेदार—इसमें हम उन रिश्तेदारों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ये संबंधी हमसे प्राथमिक संबंधियों द्वारा संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ-बहनोई-साले में संबंध, दादा-पोते में संबंध, चाचा-भतीजे में संबंध, देवर-भाभी में संबंध इस श्रेणी के संबंधों के उदाहरण हैं। मरडोक (Murdock) ने 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार बताए हैं।
- तृतीयक नातेदार—इस श्रेणी में उन,नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं अर्थात् हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी है। उदाहरणार्थ-साले की पत्नी, साले का लड़का, पड़दादा हमारे तृतीयक नातेदार हैं। मरडोक ने 151 ऐसे संबंधियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार हम चातुर्थिक, पांचमिक इत्यादि संबंधों की चर्चा करते हैं।
नातेदारी की रीतियाँ
नातेदारी की रीतियाँ विभिन्न नातेदारों से हमारे संबंधों को व्यक्त करती है तथा इनसे हमें उनके साथ होने वाले व्यवहार का पता चलता है। अन्य शब्दों में, नातेदारी की रीतियों का संबंध दो संबंधियों के बीच संबंधों तथा व्यवहार से है। नातेदारी की निम्नांकित प्रमुख रीतियाँ हैं-
- परिहार सम्बन्ध-परिहार नातेदारी की वह रीति है जो दो नातेदारों को दूरी बनाए रखने तथा प्रत्यक्ष या आमने-सामने के संबंध स्थापित न करने पर बल देती है। भारतीय समाज में ससुर-बहु संबंध या भारतीय जनरीतियों में सास-दामाद संबंध इस श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं।।
- माध्यमिक संबोधन-इस रीति में किसी नातेदार को संबोधित करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया जाता है। जिन संबंधियों के नाम पुकारना अच्छा नहीं समझा जाता, उनमें यह रीति प्रचलित है। उदाहरणार्थ-गाँव में पत्नी अपने पति का नाम न लेकर उसे पुकारने के लिए बच्चे को माध्यम बनाती है। उसका पति को ‘राजू के पिता’ कहना यह रीति प्रदर्शित करता है।
- परिहास संबंध-नातेदारी की यह रीति परिहार का विपरीत रूप है अर्थात् इसमें दो नातेदारों के बीच मधुर एवं हँसी-मजाक के संबंधों पर बल दिया जाता है। इसमें दूसरे पक्ष को छेड़ना, तंग करना तथा हँसी-मजाक करना सम्मिलित है। देवर-भाभी, जीजा-साली, साले-बहनाई में सबंध इस श्रेणी के संबंधों के मुख्य उदाहरण हैं।
- मातुलेय–इस रीति में मामा-भानजे या भानजी के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। यह रीति मातृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित है तथा इसमें बच्चों पर पिता से मामा का अधिकार अधिक होता है। संपत्ति का उत्तराधिकार भी भानजे-भानजी को होता है। अत: इस रीति में ममता का स्थान सर्वोपरि है।
- पितृश्वसेय—इस रीति में पितृश्वसा अर्थात् पिता की बहन (बुआ) का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। बुआ को माता से अधिक सम्मान दिया जाता है तथा बच्चों के विवाह भी बुआ ही कराती है। बच्चे बुआ की संपत्ति के अधिकारी होते हैं।
- सहकष्टी–इसे सहप्रसविता भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध प्रसव काल से है। इसमें पति से प्रसवा स्त्री के समान व्यवहार करने अर्थात् कष्ट प्रदर्शित करने की आशा की जाती है। जिस प्रकार का भोजन प्रसवी को मिलता है वैसा ही पति को दिया जाता है। उसे भी अलग कमरे में रखा जाता है तथा प्रसव अवधि के लिए अछूत माना जाता है।
प्रश्न 6.
राजनीतिक संस्थाएँ क्या हैं? समाज में इनका क्या महत्त्व है?
या
राज्य किसे कहते हैं? इसके प्रमुख कार्य कौन-से हैं?
या
राज्य को परिभाषित कीजिए तथा सरकार से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
आज समाजशास्त्र में समग्र समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। व्यवस्था से अभिप्राय विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर्संबंध से बना वह क्रमबद्ध ताना-बाना है जिसमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे इकाइयाँ एक-दूसरे से इस प्रकार संबंध होती हैं कि एक भाग में परिवर्तन दूसरे भाग को प्रभावित करता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के दो पहलू होते हैं—संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक। इन्हें समाज की संरचनात्मक उप-व्यवस्थाएँ तथा प्रकार्यात्मक उप-व्यवस्थाएँ भी कहते हैं। ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ समाज की प्रकार्यात्मक समस्याओं से संबंधित हैं अथवा इन्हें समाज की पूर्वपेक्षाओं से संबंधित माना जाता है।
समाज की चार प्रकार्यात्मक समस्याएँ या पूर्वापेक्षाएँ हैं: अनुकूलन, लक्ष्य-प्राप्ति, एकीकरण तथा प्रतिमानात्मक स्थायित्व एवं तनाव-नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाज को अपना अस्तित्व एवं संतुलन बनाए रखने के लिए भौगोलिक तथा सामाजिकै सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन करना पड़ता है। इस अनुकूलन हेतु प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की यांत्रिकी पायी जाती है। अनुकूलन से संबंधित प्रकार्यात्मक उप-व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं जो कि आर्थिक संस्थाओं से संबंधित है। इसमें मुख्यतः सम्पत्ति, श्रम-विभाजन, विनिमय एवं बाजार तथा विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है।
सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाज की दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या संबंधी पूर्वापेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति है। इसके अनुरूप जो प्रकार्यात्मक उप-व्यवस्था होती है उसे राज-व्यवस्था कहते हैं जो कि राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से राज्य तथा सरकार को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा ही लक्ष्यों का निर्धारण होता है और लक्ष्यों के बीच साधनों का वितरण होता है। एकीकरण की समस्या के अनुरूप प्रत्येक सामाजिक व्येवस्था में धार्मिक एवं कानूनी उप-व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। इनका संबंध क्रमशः धार्मिक एवं वैधानिक संस्थाओं से है। धार्मिक संस्थाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान धर्म को दिया जाता है। प्रतिमानात्मक स्थायित्व एवं तनाव-नियंत्रण संबंधी समस्या के समाधान हेतु शैक्षिक एवं नातेदारी उप-व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार, सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाज को बनाए रखने के लिए आर्थिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा धार्मिक संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
राजनीतिक संस्थाओं का अर्थ
राजनीतिक संस्थाओं का वृहद् अध्ययन राजनीतिशास्त्र में किया जाता है। चूंकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक जीवन की अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। राजनीतिक संस्थाओं का संबंध शक्ति के वितरण से है तथा इनके द्वारा ही समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है और यदि सभी व्यक्ति ऐसा करने लगे तो सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। शांति तथा नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का महत्त्व सभी युगों में रहा है और आज भी है। व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में व्यवस्था, प्रगति व शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्थाओं एवं समितियों पर ही है।
बॉटोमोर के अनुसार राजनीतिक संस्थाएँ समाज में शक्ति के वितरण से संबंधित हैं। इस संदर्भ में, राज्य के बारे में वेबर का विचार है कि राज्य एक ऐसा मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा में भौतिक बल के वैज्ञानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है और जो इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण अभिकरण है। जिसके कार्य कानून द्वारा किए जाते हैं। राज्य संपूर्ण समाज नहीं अपितु समाज की एक संस्था मात्र है।
राजनीतिक संस्थाओं का महत्त्व
राजनीतिक संस्थाओं की समाज तथ व्यक्तियों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था के रूप में राज्य की एक प्रमुख प्रकार्यात्मक समस्या, लक्ष्य-प्राप्ति का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। राज्य तथा सरकार द्वारा केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किए जाते अपितु इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनिवार्य साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। राजनीतिक संस्थाएँ ही समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। राज्य, सरकार तथा कानून के डर से ही सभी नागरिक सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते उनको राज्य दंडित करता है। राज्य एक सर्वशक्तिशाली संस्था है तथा इसे व्यक्ति का जीवन लेने अर्थात् उसे मृत्युदंड तक देने का अधिकार प्राप्त होता है। आर्थिक साधनों की प्राप्ति हेतु होने वाली होड़ को भी राजनीतिक संस्थाएँ ही नियमित करती है। शैक्षिक उप-व्यवस्था एवं अन्य उप-व्यवस्थाओं को दिशा-निर्देश देने का कार्य भी राजनीतिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार, राजनीतिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था तथा इसकी निरंतरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
राज्य का अर्थ एवं परिभाषाएँ
समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि शक्ति के वितरण तथा इसके प्रयोग के एकाधिकार से संबंधित है। राज्य का अर्थ जानने के लिए राज्य की परिभाषाओं का विश्लेषण करना अनिवार्य है। इसकी प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं-
- गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin}.के अनुसार-“एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के प्रभुता-संपन्न राजनीतिक संगठन को हम राज्य कहते हैं।”
- रौसेक (Roucek) के अनुसार-“संपूर्ण समाज के संदर्भ में, राज्य लोगों को ऐसी समिति है जो राजनीतिक उद्देश्यों से बनाई जाती है।”
- मैकाइवर (Maclver) के अनुसार-“राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून द्वारा शासनतंत्र से क्रियांवित होती है और जिसे निश्चित भू-प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं।”
- फेयरचाइल्ड (Fairchild) के अनुसार-“राज्य समाज की वह संस्था, पहलू या माध्यम है जो कि बल प्रयोग की सामर्थ्य एवं अधिकार रखती है, अर्थात् जो बलपूर्वक नियंत्रणं लागू कर सकती है। यह सामर्थ्य समाज के सदस्यों को नियंत्रित करने के काम भी आ सकती है और अन्य समाजों के विरुद्ध भी।”
- जिसबर्ट (Gisbert) के अनुसार-“राज्य कानून एवं राजनीतिक मामले में अपील की सबसे अंतिम अदालत है; अत: यह प्रभुसत्ताशाली एवं एक अर्थ में निरपेक्ष है।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित एक राजनीतिक संगठन है। इस राजनीतिक संगठन का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। राज्य का काम चलाने के लिए शासनतंत्र या सरकार होती है, जो राज्य का संस्थात्मक पहलू है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है। राज्य के सभी नियमों का पालन करना उस राज्य के सदस्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, तब राज्य अपनी प्रभुसत्ता के आधार पर दंड देने का अधिकार रखता है। ऎसेक (Roucek) ने ठीक ही लिखा है कि “क्योंकि सरकार की सारी शक्ति व्यक्तियों के हाथ में ही निहित रहती है तथा वे ही उसका प्रयोग करते हैं अतः सरकार की संस्था बिना, राज्य की धारणा की कोई वास्तविकता नहीं।’
इस प्रकार, समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि अन्य संस्थाओं से भिन्न है। इस संस्था के पास शक्ति भी होती है और उस शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी। इसी आधार पर राज्य प्रत्येक नागरिक को अपना मत मनवाने को बाध्य कर सकता है। जो विद्वान संस्था को एक समिति मानते हैं वे भी इस बात से सहमत हैं कि इस समिति का संस्थागत रूप राज्य के कानून एवं व्यवस्थाएँ होती हैं।
राज्य के प्रमुख कार्य
मैकाइवर ने राज्य के कार्यों की विवेचना निम्नांकित प्रकार से की है-
- वे कार्य जिन्हें केवल राज्य ही कर सकता है-कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना केवल राज्य के वश की ही बात है क्योंकि राज्य के पास शक्ति होती है तथा उसे इस शक्ति का प्रयोग । करने का पूरा अधिकार होता है। राज्य ही सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले कानूनों को निर्माण करता है, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान जीवन-अवसर प्रदान करता है तथा सबको समान सुविधाएँ प्रदान करता है। सार्वजनिक न्याय का कार्य भी राज्य द्वारा ही किया जाता है।
- वे कार्य जिन्हें राज्य कर ही नहीं सकता-ये वे कार्य हैं जिन्हें राज्य करने में असमर्थ है। उदाहरणार्थ-राज्य जनमत पर नियंत्रण नहीं कर पाता। राज्य व्यक्तियों की नैतिकता पर भी नियंत्रण नहीं लगा सकता। राज्य व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार पर रोक लगाने हेतु कानून पारित कर सकता है, परंतु व्यक्ति किस सीमा तक उन कानूनों का पालन करेंगे, यह एक दूसरी बात है।
- वे कार्य जिन्हें राज्य अच्छी प्रकार से कर सकता है–ये वे सामाजिक कार्य हैं जिन्हें राज्य के अतिरिक्त कोई अच्छी समिति या संस्था नहीं कर सकती अपितु राज्य इन्हें अन्य समितियों एवं संस्थाओं के मुकाबले बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है। राज्य अपने साधनों से प्राकृतिक साधनों का सर्वाधिक शोषण करता है। वनों, खानों तथा सीमाओं इत्यादि की सुरक्षा राज्य से अच्छी कोई नहीं कर सकता। राज्य सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है प्रतियोगिता को नियमित करता है। सभी नागरिकों का समान कल्याण राज्य से बेहतर कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती है।
- वे कार्य जिन्हें राज्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है-वे वे कार्य हैं जो राज्य द्वारा ठीक प्रकार नहीं किया जा सकते। अन्य समितियाँ एवं संस्थाएँ इन्हें राज्य से ज्यादा अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरणार्थ-राज्य हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति धार्मिक संस्थाओं द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से की जा सकती है। राज्य से व्यक्ति उतना अपनत्व प्राप्त नहीं कर पाता जितना उसे व्यक्तिगत, धार्मिक व आर्थिक संस्थाओं एवं समितियों से मिल सकता है।
राज्य तथा सरकार में अंतर
अधिकतर विद्वान राज्य को एक समिति मानते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि राज्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ संस्थागत नियमों को मान्यता देता है। सरकार समिति का संस्थागत पक्ष है। यद्यपि सरकार का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही होता है तथापि सरकार स्वयं अपने आप में एक व्यवस्था है। क्योंकि यह नियमबद्धता एवं निश्चित कार्यप्रणाली से संबद्ध होती है। सरकार राज्य की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था के रूप में कार्य करती है। एण्डरसन तथा पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार सरकार तीन प्रकार के प्रमुख कार्य करती है—वैधानिक या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य तथा न्यायपालिका संबंधी कार्य।।
राज्य तथा सरकार में निम्नलिखित प्रमुख अंतर पाए जाते हैं-
- राज्य व्यक्तियों का एक विशाल राजनीतिक संगठन है जिसका निर्माण निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंदर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है अर्थात् राज्य की परिधि सीमित होती है। इसके विपरीत, सरकार एक संस्था है अर्थात् यह वह साधन है जिसके द्वारा राज्य अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करता है।
- राज्य बहुत-कुछ स्थायी होता है, जबकि सरकार में परिवर्तन होता रहता है। अन्य शब्दों में, राज्य अपेक्षाकृत स्थायी होता है, जबकि सरकार परिवर्तनशील होती है।
- राज्य एक साध्य है, जबकि सरकार उस साध्य को प्राप्त करने का एक साधन-मात्र है।
- राज्यों की आधारभूत विशेषताएँ एकसमान हो सकती हैं, परंतु दो राज्यों की सरकारों में पूरी तरह से समानता नहीं पाई जाती है।
प्रश्न 7.
आर्थिक संस्थाएँ क्या हैं तथा समाज में इनका क्या महत्त्व है?
या
आर्थिक संस्थाओं को परिभाषित कीजिए तथा प्रमुख आर्थिक संस्थाओं को विस्तार में समझाइए।
या
आर्थिक संस्थाएँ क्या हैं एवं उनके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं?
उत्तर
मानव के जन्म के साथ ही उसे अनेक आवश्यकताएँ घेर लेती हैं। इनमें से कुछ आवश्यकताएँ उसकी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं; जैसे कि भोजन, वस्त्र तथा निवास की; और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ उत्पादन, विनिमय, वितरण से संबंधित होती है। आर्थिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। आर्थिक संस्थाएँ मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करती हैं। यदि मानवीय आवश्यकताएँ; विशेषकर भौतिक आवश्यकताएँ बिना नियमों के संघर्ष से प्राप्त होने की स्थिति में आ जाएँ तो सामाजिक संरचना ही नष्ट हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मत है कि आर्थिक संस्थाओं को समाज में केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। यहाँ पर आर्थिक संस्था व आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में यह बताना आवश्यक है कि ‘आर्थिक व्यवस्था’ एक विस्तृत धारणा है, जबकि ‘आर्थिक संस्था’ सीमित धारणा है।
आर्थिक संस्था का अर्थ एवं परिभाषाएँ
आर्थिक संस्थाओं का संबंध समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या से होता है। इनमें उन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो समाज में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होती है। आर्थिक संस्थाओं द्वारा ही जीवन निर्वाह से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रमुख विद्वानों ने आर्थिक संस्था की परिभाषाएँ निम्नांकित प्रकार से दी हैं-
- एण्डरसन एवं पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार-“वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के माध्यम से आर्थिक संस्थाएँ समाज के अस्तित्व को बनाए रखती हैं। यह कार्य, पूँजी, श्रम, भूमि, कच्चे माल तथा व्यवस्था संबंधी योग्यता के अधिकतम उपयोग द्वारा संभव होता है।”
- जोंस (Jones) के अनुसार—“आर्थिक संस्थाएँ विभिन्न प्रविधियों, विचारों तथा प्रथाओं की उस समग्रता को कहते हैं जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक पर्यावरण के अधिकतम उपभोग से संबंधित हैं।”
- डेविस (Davis) के अनुसार-समाज चाहे सभ्य हो या असभ्य, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत विचारों, आदर्श नियमों तथा पदों को आर्थिक संस्था की संज्ञा दी जाएगी।
आर्थिक संस्थाओं की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आर्थिक संस्थाएँ अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादन तथा वितरण के नियमों का विवेचन करती है। समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद, सामन्तवाद, संपत्ति श्रम-विभाजन तथा अनुबंध (Contract) इत्यादि प्रमुख आर्थिक संस्थाएँ हैं। अर्थव्यवस्था को हम चार प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं-
- संग्रहकारी अर्थव्यवस्था
- सरल रूपान्तरकारी अर्थव्यवस्था
- जटिल रूपान्तरकारी अर्थव्यवस्था तथा
- मिश्रित अर्थव्यवस्था।
आर्थिक संस्थाओं का महत्त्व
किसी भी समाज के आर्थिक संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः आर्थिक संस्थाएँ किसी समाज की उस प्रकार्यात्मक उप-व्यवस्था का निर्माण करती हैं जो समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या को हल करती है। इसलिए अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संस्थाओं को कई बार अनुकूलनकारी उप-व्यवस्था भी कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में लगी सभी । इकाइयों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का कार्य आर्थिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्हीं से ऐसी सुविधाएँ उत्पन्न होती हैं जो सामान्य रूप से परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि के लिए आवश्यक होती हैं। इन्हीं संस्थाओं द्वारा कोई भी समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करता है तथा प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है।
आर्थिक संस्थाओं की प्रकृति पूर्व-औद्योगिक तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। पूर्व-औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भूमि ही धन का स्रोत होती है, जीवंत शक्ति का अत्यधिक प्रयोग होता है, सरल प्रौद्योगिकी पायी जाती है, श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण का निम्न स्तर पाया जाता है, प्रत्यक्ष एवं परंपरागत विनिमय तथा वितरण द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तथा अधिकतर प्रबंध का आधार परिवार ही होती है। इसलिए इन समाजों में संपत्ति तथा विनिमय संबंधी आर्थिक संस्थाओं की ही प्रमुखता होती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संस्थाएँ विकसित श्रम-विभाजन, उत्पादन, व्यापार एवं लाभ तथा अप्रत्यक्ष विनिमय व वितरण से संबंधित होती हैं। क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इन्हीं विशेषताओं की प्रमुखता पाई जाती है।
समाज की विभिन्न उप-व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य साधन आर्थिक उप-व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इस उप-व्यवस्था, जिसमें आर्थिक संस्थाएँ भी सम्मिलित होती हैं, की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
आर्थिक संस्थाओं के प्रमुख प्रकार
आर्थिक संस्थाएँ अनेक प्रकार की होती हैं। समाजशास्त्र में निम्नलिखित पाँच आर्थिक संस्थाओं को प्रमुख माना जाता है-
(अ) समाजवाद
समाजवाद व्यक्तिगत पूँजी को सार्वजनिक पूँजी में बदलकर, प्रतियोगिता की मात्रा को कम कर अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने पर बल देता है। इस वाद का जन्म, पूँजीपतियों द्वारा शोषण तथा वर्ग-संघर्ष के विरुद्ध हुआ है। रोबर्ट ओवन, सेंट साइमन आदि विचारकों ने इसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास किया था, परंतु साधनों की अनिश्चिता ने इस वाद को पनपने नहीं दिया। समाजवाद के संदर्भ में रेमजे मैक्डानल्ड का विचार है कि साधारण अर्थों में समाजवाद की परिभाषा यही है कि उसका उद्देश्य समाज के आर्थिक व भौतिक साधनों का संगठन करना तथा मानव साधनों के द्वारा उनका नियंत्रण करना है। समाजवाद मानव मूल्यों की रक्षा करने में सहायता करता है। आज हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रधानता दी जा रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संस्थाएँ भिन्न प्रकार की होती है। समाजवाद के कई रूप समाजों में प्रचलित हैं।
(ब) साम्यवाद
कुछ विद्वानों ने साम्यवाद को व्यवहारिकता की कमी के कारण मात्र विचारधारा निरूपित किया है। जिन विद्वानों ने साम्यवाद को प्रोत्साहन दिया है उनमें मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन आदि प्रमुख हैं। साम्यवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य के अधिकार होते हैं। ऐसी संपत्ति, जो बिना श्रम से मिली हो, का उपभोग करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है। इस ‘वाद’ में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्त्व मिलता है। साम्यवादी व्यवस्था समानता को मानती है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि गंभीर संकट के समय व्यक्ति की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा ले। साम्यवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक व आर्थिक संरचना बदलने के लिए हिंसा का बुरा नहीं मानती है। अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माध्यम उचित है। इस ‘वाद’ के अंतर्गत धर्म का कोई महत्त्व नहीं है।
(स) पूँजीवाद
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य कानूनी तौर पर संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व पर विश्वास रखता है। अर्थात् पूँजीवाद, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को पूर्ण समर्थन करता है। पूँजीवाद, धन के संग्रह, प्रतियोगिता वं आर्थिक स्वतंत्रता को प्रश्रय देता है। बूचर के अनुसार, “पूँजीवाद का आवश्यक गुण उसके उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं में पाया जाने वाला संबंध है। कुछ विद्वानों ने पूँजीवाद को एक ऐसी अर्थव्यवस्था माना है जिनमें सभी व्यक्तियों को काम करने का अवसर प्राप्त हो, सभी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हों तथा सभी अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतियोगिता कर सकें।
(द) संपत्ति संपत्ति
एक आर्थिक संस्था है जिसका संबंध वितरण व्यवस्था का स्थिर पहलू है। संपत्ति से अभिप्राय किसी भी वस्तु पर स्वामित्व एवं अधिकार से हैं। डेविस (Davis) के अनुसार, “संपत्ति वास्तव में वितरण-व्यवस्था का स्थिर पहलू है। इसमें कुछ सीमित वस्तुओं के प्रति समस्त व्यक्तियों एवं समूहों के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों (स्वामी) के अधिकार व उसके कर्तव्य सम्मिलित हैं। इसी भाँति, हॉबहाउस (Hobhouse) के अनुसार, “संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण से है, ऐसा नियंत्रण जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जो कम या अधिक किसी-न-किसी अंश में स्थायी तथा पूर्ण होता है। अतः संपत्ति भौतिक एवं अन्य वस्तुओं से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की एक व्यवस्था है।
(य) श्रम-विभाजन
श्रम-विभाजन का प्रमुख आर्थिक संस्था है परंतु दुर्णीम (Durkheim) ने अपने अध्ययन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि श्रम-विभाजन एक सामाजिक तथ्य भी है। श्रम-विभाजन की उत्पत्ति आधुनिक नहीं है क्योंकि प्राचीन समाजों में भी यह कुछ-न-कुछ मात्रा में पाया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में श्रम-विभाजन के सिद्धांत को सामाजिक दृष्टिकोण से देखने के प्रयास शुरू हुए। एडम स्मिथ (Adam Smith) प्रथम विद्वान थे जिन्होंने श्रम-विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया परंतु श्रम-विभाजन केवल आर्थिक जगत तक ही सीमित नहीं है अपितु आज समाज के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। आज राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्य अधिकाधिक विशेषीकृत होते जा रहे हैं। स्मिथ ने श्रम विभाजन को आर्थिक घटना के रूप में देखते हुए इसके दो प्रमुख परिणामों-उत्पादन में वृद्धि तथा वस्तुओं की श्रेणी में श्रेष्टता का उल्लेख किया परंतु दुर्णीम ने श्रम-विभाजन को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हुए इसके प्रमुख सामाजिक परिणाम-समाज में एकता बनाए रखने पर बल दिया।
फेयरचाइल्ड (Fairchild) द्वारा सम्पादित समाजशास्त्र एवं संबंधित विज्ञानों के शब्दकोश में श्रम-विभाजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “श्रम-विभाजन किसी भी समाज में पूरे किए जाने ब्राले कार्यों और सेवाओं का उन लोगों के मध्य वितरण और विभेदीकरण है, जिन्हें वास्तव में उन्हें पूरा करना है।”
जॉनसन (Johnson) श्रम-विभाजन को स्पष्ट करके हुए सरल शब्दों में लिखते हैं, “हमारे समाज में, एक मैराज मैकेनिक से यह उम्मीद नहीं की जाती है वह इलैक्ट्रीशियन का स्थान ले लेगा; प्रत्येक अपनी भूमिका अलग रखता है जो ‘स्थायी’ सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त, तकनीकी दृष्टि से कुशलताओं को विशिष्टीकृत संकुल है। इस भूमिका के साथ इसके अनुरूप दायित्व और सुस्पष्ट अलग प्रस्थिति (Status) जुड़े हैं। इसी अर्थ में हम श्रम-विभाजन की बात करेंगे।”
इस भाँति, हम देखते हैं श्रम-विभाजन केवल विशुद्ध संस्था ही नहीं रह जाती बल्कि उसके महत्त्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी हमारे सामनेउजागर हो जाते हैं क्योंकि श्रम-विभाजन द्वारा प्रस्थितियों की सृजन होता है और वह सृजन समाज में न केवल विभेदीकरण बढ़ाता है बल्कि समाज के संस्तरण को भी एक अलग आधार प्रदान करता है। परिणामतः सामाजिक संस्तरण में जटिलता की वृद्धि होती है। किसी समाज में जितना अधिक श्रम-विभाजन होता जाएगा उतना ही वह समाज जटिलं होता चला जाएगा। अमेरिका में ‘श्रम-विभाजन (1949)’ में व्यवसायों के विभिन्न शीर्षकों अर्थात् नामों का शब्दकोश प्रकाशित किया। हम आश्चर्य करेंगे कि हम उसमें 22,000 व्यवसायों का जिक्र पाते हैं जो समाज द्वारा वैधता प्राप्त है। यह आधुनिक, उन्नत एवं औद्योगिक समाज की जटिलता का लक्षण है। समाजशास्त्रियों के लिए श्रम-विभाजन में रुचि लेना और इसका अध्ययन करना स्वाभाविक ही है।
प्रश्न 8.
धर्म का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामाजिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है?
या
धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म के प्रमुख तत्त्व कौन-कौन से हैं। समझाइए।
उत्तर
प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति धर्म (Religion) से अनिवार्य रूप से परिचित होता है तथा किसी-न-किसी रूप में अपने जीवन में धार्मिक क्रियाओं को भी संपन्न करता है, परन्तु फिर भी ‘धर्म का अर्थ एकाएक स्पष्ट कर देना प्रायः सरल नहीं होता। ‘धर्म की अवधारणा एक जटिल एवं बहुपक्षीय अवधारणा है अतः इसका वर्णन कुछ सीमितं शब्दों में करना प्रायः कठिन होता है। यूँ तो विश्व में अनेक धर्मों की स्थापना हुई परंतु वास्तव में धर्म एवं धार्मिक प्रवृत्ति सब कहीं एक-समान ही है, अंतर केवल बाहरी रूप को है। धर्मों को अलग-अलग नाम देना धर्मवाद का प्रतीक है।
धर्म का अर्थ एवं परिभाषाएँ
धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन’ (Religion) कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के ‘rel (Digio’ नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ‘बाँधना’। इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में ‘धर्म’ का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक-दूसरे से बाँधते या जोड़ते हैं। अन्य शब्दों में, धर्म मनुष्य की युगों से विद्यमान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान के प्रति होती है। विभिन्न विद्वानों ने धर्म को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है-
- मैलिनोव्स्की (Malinowsk) के अनुसार-“धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी; और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ-साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है।”
- फ्रेजर (Frazer) के अनुसार-“धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ, जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव-जीवन को मार्ग दिखलाती है और नियंत्रित करती हैं।”
- टॉयलर (Tylor) के अनुसार-“आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म हैं। से सत्ताएँ दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं।”
- जॉनसन (Johnson) के अनुसार-“धर्म कम या अधिक रूप में उच्च अलौकिक व्यवस्था या प्राणियों, शक्तियों, स्थानों एवं अन्य तत्त्वों के संबंध में विश्वासों एवं व्यवहारों की एक स्थिर | प्राणाली है।”
- हानिगशीम (Honigsheim) के अनुसार-“प्रत्येक मनोवृत्ति, जो कि इस विश्वास पर आधारित या संबंधित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और उनसे संबंध स्थापित करना संभव व महत्त्वपूर्ण है, धर्म कहलाती है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म को किसी-न-किसी रूप में अतिमानवीय शक्ति में विश्वास के रूप में स्पष्ट किया गया है। यह जीवन का सत्य और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। मजूमदार एवं मदन (Majumdar and Madan) ने लिखा है, “धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर तथा अनुकूलन का वह प्रकार है जो लोगों के लिए अलौकिक है, शक्ति के अर्थ से प्रभावित होता है।”
धर्म के प्रमुख तत्त्व । धर्म का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनके बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस पर भी विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् कुछ ऐसी बातें या तत्त्व अवश्य हैं जिन पर विद्वानों में बहुत कम मतभेद है। धर्म के ये तत्त्व निम्नलिखित हैं-
- संवेगात्मक भावनाएँ–पवित्र विश्वासों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका संवेगात्मक भावनाओं की होती है। प्रेम और भय इनके प्रमुख आधार हैं। एक व्यक्ति प्रेम विभोर होकर ईश्वर में श्रद्धा रखता है तो दूसरा दैवी विपत्तियों के भय से ईश्वर या भूतों की उपासना करता है।
- धर्माचरण–प्रत्येक धर्म में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ रीतियाँ तथा विधियाँ होती हैं। इन रीतियों और विधियों को ही आराधना कहा जाता है। आराधना का मूल उद्देश्य ईश्वरे या देवताओं को प्रसन्न करना होता है जिससे आराधना करने वाले को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। प्रत्येक धर्म में आराधना करने के लिए अलग-अलग ढंग होते हैं।
- पवित्र विश्वास–मानवीय ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) प्राकृतिक तथा (ख) पवित्र। प्राकृतिक घटनाओं को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं; जैसे–बिजली का गिरना, भूकंप या भूचाल, पेड़, नदी आदि। इनका स्वरूप पूर्णतया इतिवृत्तात्मक होता है। दूसरे प्रकार की घटनाएँ पवित्र घटनाएँ होती हैं, जिनको प्रत्यक्ष या वैषयिक रूप से नहीं समझा जा सकता। इस कोटि की घटनाएँ ही धर्म का मूल आधार होती हैं। किस घटना को प्राकृतिक विश्वास की श्रेणी में रखा जाए और किस घटना को पवित्र विश्वासों में, यह समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए—पीपल का पेड़ कुछ व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक घटना मात्र है, क्योंकि वह केवल पेड़ हैं, परंतु हिंदुओं के लिए पीपल’ एक पूजा योग्य पवित्र वृक्ष है। इसी प्रकार ‘गंगा’ कुछ व्यक्तियों के लिए नदी मात्र है तो कुछ के लिए पवित्र स्थान।
- धर्म के प्रतीक-प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था को प्रकट करने के लिए प्रतीक निर्धारित कर लिए जाते हैं। वास्तव में ये प्रतीक अमूर्त तथ्यों का मूर्त प्रतिपादन होते हैं, जैसे कि कुछ वस्तुएँ एवं स्थान (तीर्थस्थान) धर्म के प्रतीक मान लिए जाते हैं।
धर्म के कार्य/भूमिका या महत्त्व
धर्म के कार्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। धर्म सदा से समाज को प्रभावित करता आया है और व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहा है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली साधन है। धर्म के सामाजिक महत्त्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है-
1. सामाजिक नियंत्रण में सहायक-धर्म का मुख्य कार्य सामाजिक नियंत्रण का रहा है। अतीतकाल से ही धर्म मनुष्यों को बताया आया है कि बुरे कार्यों का परिणाम बुरा ही होता है। और भले कार्यों का अच्छा। धर्म के प्रभाव के कारण ही दुश्चरित्र एवं भ्रष्ट व्यक्तियों ने बुरे कार्यों का परित्याग कर दिया और लोग प्रेम, सहयोग और परोपकार के जीवन या व्यवहार को विशेष महत्त्व देने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में धर्म के दो स्वरूप हो गए—
- भय का धर्म, जो व्यक्ति को बुरे तथा पापपूर्ण कृत्य करने से रोकता था;
- विश्वास को धर्म, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करता था तथा समाज में प्रेम और सहयोग के साथ जीवन व्यतीत करता था।
विश्व के समस्त धर्म किसी-न-किसी रूप में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। धर्म द्वारा लागू किया गया सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण होता है तथा विश्व के समस्त धर्म किसी-न-किसी रूप में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। धर्म द्वारा लागू किया गया सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक नियंत्रण होता है तथा बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। धर्म द्वारा लागू किए गए सामाजिक नियंत्रण की सामान्य रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसके साथ अलौकिक सत्ता तथा पाप-पुण्य एवं लोक-परलोक तथा पुनर्जन्म की धारणा जुड़ी रहती है। अतः धर्म मानव-व्यवहार को नियंत्रित
करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता रहा है।
2. नैतिकता का आधार-धर्म को यदि नैतिकता का आधार कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। धर्म और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक समाज की नैतिकता का आधार धर्म होता है। धर्म बताता है कि अनैतिक कार्यों का परिणाम बुरा होता है तथा बुरा काम करने वाले को नरक मिलता है। इन विचारों से भी सामाजिक नियंत्रण में सहायता मिलती है।
3. संस्कृति का अंग–धर्म और संस्कृति में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अन्य शब्दों में, धर्म संस्कृति का एक अंग होता है और इसके माध्यम से ही समाज अपनी संस्कृति का प्रचलन करता है। संस्कृति द्वारा धर्म का निर्धारण होता है।
4. सामाजिक एकता में वृद्धि करना-एक धर्म के मानने वाले समय-समय पर एक धार्मिक स्थल पर मिलते-जुलते रहते हैं तथा एक-सी परंपराओं में विश्वास करते हैं; अत: उनके अन्दर एकता तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। दुर्णीम के अनुसार, धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य सामाजिक एकता बनाए रखना है।
5. मानसिक तनाव को कम करना-इस संसार में.प्रत्येक व्यक्ति को अनेक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इन संकटों के कारण मस्तिष्क में अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये तनाव मनुष्य में निराशा उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसी दशा में व्यक्ति को कोई सहारा न मिले तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। धर्म निराश और टूटे दिलों को सहारा देता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। ईश्वर-भरोसे सब-कुछ छोड़कर मनुष्य निश्चित हो जाता है।
6. कल्याणकारी भावनाओं को प्रोत्साहित करना-प्रत्येक धर्म परोपकार, दान, दया को महत्त्व देता है। धार्मिक भावनाएँ ही धनिकों को धर्मशाला, विश्राम-गृह, विद्यालय तथा औषधालय आदि बनवाने के लिए उत्साहित करती हैं। इस प्रकार धर्म समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए सर्वसाधारण को उत्साहित करता है।
7. परिवार की एकता को सुदृढ़ करना-धर्म परिवार को एकता के सूत्र में बाँधता है। एक परिवार के सभी सदस्य एक-सी धार्मिक क्रियाएँ करते हैं, एक ही देवी-देवता की पूजा करते हैं। तथा धार्मिक-समारोह मनाते हैं। धर्म ही विवाह, आचरण और पिता-पुत्र, पति-पत्नी के संबंधों पर प्रकाश डालता है।
8. कलात्मक विकास में योगदान देना-धर्म का कला के विकास में अपना विशेष योगदान रहा है। धर्म से प्रेरित होकर अनेक काव्य और कथा-ग्रंथों की रचना हुई। इसी प्रकार अनेक मंदिरों, मस्जिदों और चर्चा का निर्माण भी धार्मिक प्रेरणाओं का फल है। धर्म-भावनाओं से प्रेरित कलाकार अत्यंत तन्मयता से सृजन कार्य में लीन होते हैं।
9. देशभक्ति की भावना का विकास-धर्म अपनी मातृभूमि से प्यार करना सिखाता है। प्रायः एक देश के वासी एक ही धर्म के मानने वाले होते हैं अतः उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है।
10. अध्यात्मवाद को प्रोत्साहित करना-धर्म व्यक्ति को बताता है कि इस संसार से परे भी कोई शक्ति होती है जो व्यक्ति को आपत्ति या संकट के समय बचा सकती है। अतः धर्म ही व्यक्ति के भौतिकता से परे हटाकर अध्यात्मवाद की ओर ले जाती है। इस प्रकार धर्म भौतिकता तथा आध्यात्मिकता में समन्वय करके संतुलन बनाए रखता है। निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि धर्म सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह नियंत्रण का एक अनौपचारिक परंतु काफी अधिक प्रभावशाली साधन माना जाता है।
प्रश्न 9.
शिक्षा किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
या
शिक्षा से आप क्या समझते हैं? मानव के सामाजिक जीवन में शिक्षा के मुख्य कार्य क्या हैं?
या
शिक्षा का सामाजिक अर्थ समझाते हुए शिक्षा की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
या
शिक्षा के सामाजिक कार्यों का संक्षेप में विवेचन कीजिए।
उत्तर
शिक्षा वास्तव में एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की निहित शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा के ही द्वारा मनुष्य प्राणी’ से इंसान या सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा का संबंध मनुष्य के जीवन के विभिन्न अथवा यह कहा जाए कि समस्त पक्षों से है। इससे मनुष्य का शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास होता है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इस अर्थ में शिक्षा मनुष्य के पूरे जीवन भर चलती रहती है। इससे भिन्न अनेक बार शिक्षा को संकुचित अर्थों में भी प्रतिपादित किया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का आशय स्कूल, पाठशाला, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में होने वाले अध्ययन-अध्यापन से होता है। यह सीमित होती है तथा एक समय पर आकर समाप्त हो जाती है। इसे औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है।
शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएँ।
शिक्षा अपने आप में एक अत्यधिक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है जो किसी-न-किसी रूप में जीवनपर्यंत चलती रहती है। इस स्थिति में शिक्षा का अर्थ भी व्यापक, बहुपक्षीय तथा कुछ हद तक विवादास्पद होना स्वाभाविक ही है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से शिक्षा के भिन्न-भिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को निर्धारित किया गया है। विद्वानों तथा शिक्षाशास्त्रियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण ने भी शिक्षा के अर्थ को विविधता प्रदान करने में योगदान दिया है। इस स्थिति में शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए विभिन्न पक्षों से शिक्षा के अर्थ का विवेचन करना प्रासंगिक होगा। मुख्य रूप से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा के प्रचलित अर्थ, शिक्षा के संकुचित अर्थ तथा शिक्षा के व्यापक अर्थ की चर्चा करना आवश्यक है।
(अ) शिक्षा का शाब्दिक अर्थ
पत्येक शास्त्र या विषय का कुछ-न-कुछ नाम रखा जाता है। यह नाम सार्थक तथा विषय के लिए परिचयात्मक होता है अतः नाम के शाब्दिक अर्थ को जान लेने से विषय के प्रति पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें ‘शिक्षा’ के अर्थ का निर्धारण करना है अत: हिंदी के शब्द ‘शिक्षा’ तथा इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द Education’ का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ जानना हमारे लिए अभीष्ट होगा।
‘शिक्षा’ का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ-हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द ‘शिक्षा’ वास्तव में संस्कृत भाषा से लिया गया है तथा संस्कृत भाषा में इसका संबंध ‘शिक्षा’ धातु से है। संस्कृत भाषा में इस धातु का आशय ज्ञान ग्रहण करने या विद्या प्राप्त करने से है। इस व्युत्पत्तिमूलक अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो ज्ञान अथवा विद्या प्राप्त करने या प्रदान करने की माध्यम है। अनेक विद्वान् शिक्षा के इसी अर्थ को स्वीकार करते हुए शिक्षा की व्याख्या एवं व्यवस्था करने के पक्ष में हैं।
“Education’ का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ-अंग्रेजी शब्द Education’ की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। विद्वानों का विचार है कि Education शब्द का संबंध लैटिन भाषा के तीन शब्दों ‘educatium (एजूकेसीयम) educere’ (एजूसीयर) तथा ‘educare’ (एजूकेयर) से है। इन तीनों ही शब्दों को लैटिन भाषा में लगभग समान अर्थ है। इन शब्दों का क्रमश: अर्थ है-विकसित करता, निकालना या आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या शिक्षित करना।
इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक या व्यक्ति को निहित शक्तियों या क्षमताओं को विकसित किया जाता है या प्रस्फुटित किया जाता है। इस प्रकार का विकास जीवन भर होता रहता है; अत: शिक्षा की प्रक्रिया भी जीवन भर चलती रहती है। स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण से शिक्षा का आशय संस्थागत शिक्षा तक सीमित नहीं है।
(ब) शिक्षा का संकुचित अर्थ
‘शिक्षा’ के सामान्य परिचय को प्रस्तुत करते समय स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है तथा इसके अर्थ को सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण से शिक्षा के संकुचित अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। इस दृष्टिकोण से शिक्षण-कार्य के लिए विधिवत् स्थापित की गई शिक्षा संस्थाओं (पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि) द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रक्रिया एक औपचारिक एवं व्यवस्थित तथा नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस अर्थ को आधार मानकर वही बालक या व्यक्ति शिक्षित माना जा सकता है जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश प्राप्त करके निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, परीक्षा में सम्मिलित होता है तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है। जे०एस० मैकेन्जी (J.S. Mackenzi) ने स्पष्ट किया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की शक्तियों के विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं के शब्दों में, “संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए सचेत रूप से किए गए किसी भी प्रयास से ही हो सकता है।”
(स) सामान्य रूप से शिक्षा का प्रचलित अर्थ
शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त उसके सामान्य रूप से प्रचलित अर्थ की भी चर्चा की जाती है। समाज में अधिकांश व्यक्ति शिक्षा के इसी अर्थ से परिचित हैं। इस अर्थ के अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित कुछ तथ्यों एवं सूचनाओं को किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लेना या एकत्र कर लेना ही शिक्षा : कहलाता है। इस दृष्टिकोण से तथ्यों के संकलन के ढंग आदि के विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जाता। तथ्य संकलन एवं सूचनाएँ एकत्र करने के ढंग उचित भी हो सकते हैं तथा अनुचित भी। शिक्षा के इस अर्थ के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति के आतंरिक विकास को कोई महत्त्व प्रदान नहीं किया गया बल्कि केवल बाहरी जगत् से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के एकत्रीकरण को ही शिक्षा माना गया है। शिक्षा के अर्थ के इस स्पष्टीकरण की पर्याप्त आलोचना की गई है। विद्वानों का कहना है कि इस व्याख्या से न तो शिक्षा की प्रक्रिया का समुचित परिचय ही प्राप्त होता है और न ही यह शिक्षा के वास्तविक अर्थ को ही स्पष्ट करने में सहायक है। इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा गया है। कि शिक्षा से आशय अंदर से होने वाले विकास से है न कि बाहर से किया जाने वाला संचय। शिक्षा की प्रक्रिया का परिचालन स्वाभाविक मूलप्रवृत्तियों तथा रुचियों की सक्रियता से होता है। अतः बाहरी शक्तियों के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को शिक्षा नहीं कहा जा सकता।
(द) शिक्षा का व्यापक अर्थ
अनेक विद्वानों ने ‘शिक्षा’ की प्रक्रिया की व्याख्या उसके व्यापक अर्थ में की है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में एक अति व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। इस रूप में शिक्षा जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन भर निरंतर चलती रहती है। काल या अवधि के ही समान इस अर्थ के अनुसार शिक्षा प्रदान करने अथवा ग्रहण करने का क्षेत्र भी सीमित नहीं होता अर्थात् शिक्षण का क्षेत्र शिक्षा संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा जगत् ही शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा प्रदान करने का क्षेत्र है। शिक्षा की इस व्यापक व्याख्या को मैकेन्जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, “विस्तृत अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है तथा जीवन के प्राय: प्रत्येक अनुभव से उसके भण्डार में वृद्धि होती है। व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करता है। ये अनुभव किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि केवल विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा संस्था के अध्यापक ही शिक्षक नहीं होते बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में शिक्षक की भूमिका निभा सकता है। जिस भी व्यक्ति से कोई नई बात सीखी जाए, वहीं व्यक्ति उस संदर्भ में शिक्षा है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर कोई बालक भी किसी प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शिक्षक सिद्ध हो सकता है। बालक ही क्या, पर्यावरण से भी अनेक बातें सीखी जा सकती हैं। अत: पर्यावरण भी हमारे लिए शिक्षक ही हैं।
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से भिन्न शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी अति व्यापक है। इसे दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, न कि विभिन्न स्तरों के प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इस तथ्य को एडलर (Adler) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है, “शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित क्रिया है, यह केवल छोटे बालकों से ही संबंधित नहीं होती है। यह तो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है।”
शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ
‘शिक्षा की परिभाषाओं के उपर्युक्त विवरण द्वारा काफी हद तक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसके और अधिक स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवर्णित हैं–
1. निरंतर चलने वाली प्रक्रिया–शिक्षा अपने आप में एक प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन का विकास होता है।
2. विकास की प्रक्रिया-शिक्षा की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों तथा निहित शक्तियों का प्रकटीकरण तथा प्रस्फुटन होता है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बाहर से कुछ भी थोपना संभव नहीं होता।
3. सचेतन प्रक्रिया–-एक दृष्टिकोण से शिक्षा को सचेतन प्रक्रिया भी स्वीकार किया गया है। शिक्षा की इस विशेषता के अनुसार, शिक्षा को जानबूझकर ग्रहण किया जाता है तथा इसके लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में काफी हद तक नियमितता भी होती है।
4. आजीवन चलने वाली प्रक्रिया जैसा की पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है; शिक्षा केवले स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन के समस्त क्षेत्र ही शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेने पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु तक किसी-न-किसी रूप में चलती ही रहती है।
5. परिवर्तनकारी प्रक्रिया–शिक्षा अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो संबद्ध व्यक्तियों के जीवन में अनेक परिवर्तन लांती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में बहुमुखी परिवर्तन आता है। शिक्षा के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर बालक की मूलप्रवृत्तियों, संवेगों, मनोवृत्तियों तथा प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं का परिमार्जन होता है, वहीं साथ-ही-साथ शिक्षा के ही प्रभाव से व्यक्ति की चिंतन प्रणाली, कार्य-प्रणाली तथा विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं के ढंग में भी परिवर्तन होता है।
6. गत्यात्मक प्रक्रिया–शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसकी एक अन्य विशेषता का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस विशेषता के अनुसार शिक्षा को एक गत्यात्मक प्रक्रिया कहा जा सकता है। गत्यात्मक से आशय है कि शिक्षा की प्रक्रिया न तो स्थिर है और न | ही जड़। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के निरंतर होने वाले विकास से है तथा विकास सदैव उन्नयनकारी होता है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया गत्यात्मक प्रक्रिया है।
7. द्विमुखी प्रक्रिया-शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कुछ विद्वानों ने इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इस विशेषता का विस्तृत विश्लेषण एवं प्रतिपादन मुख्य रूप से प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एडम्स (Adams) ने किया है। सर्वप्रथम एडम्स ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जो एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। एडम्स के ही शब्दों में, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जिससे उसके विकास में परिवर्तन हो जाए।” यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक के प्रयासों के द्वारा बालक के व्यवहार एवं विकास में परिवर्तन आता है। सामान्य रूप से शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, ज्ञान के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके भी बालक के विकास को प्रभावित किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया को जब द्विमुखी प्रक्रिया कहा जाता है तब शिक्षा का एक ध्रुव (Pole) शिक्षक होता है तथा दूसरा ध्रुव बालक होता है।
8. त्रिमुखी प्रक्रिया-कुछ विद्वानों ने शिक्षा की प्रक्रिया में निहित प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए इसको एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। इस मान्यता के अनुसार शिक्षा के तीन अंग हैं–शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा बालक। इस मान्यता के अनुसार ‘शिक्षक’ तथा ‘बालक’ के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए जॉन डीवी ने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की है। डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ-ही-साथ सामाजिक पक्ष का भी समान रूप से महत्त्व है। शिक्षा की प्रक्रिया सदैव समाज में रहकर ही चलती है। समाज से बिलकुल अलग रहकर शिक्षा की प्रक्रिया का चल पाना संभव नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि समाज के सहयोग से ही बालक को मनोवैज्ञानिक विकास भी सुचारू रूप से हो सकता है। इस प्रकार, शिक्षा द्वारा बालक का सामाजिक विकास भी होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है। कि बालक को उस समाज के लिए शिक्षित करना चाहिए, आगे चलकर जिस समाज को उसे सदस्य बनना है। यह तभी हो सकता है जबकि बालक की शिक्षा समाज के ही माध्यम से हो। समाज द्वारा ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में बालक को कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए तथा पढ़ाने के लिए किस-किस शिक्षण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि बालक की कार्यकुशलता में वृद्धि हो तथा वह समाज द्वारा स्वीकृत आचरण करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार बालकों को शिक्षित करता है। इसी व्याख्या के आधार पर शिक्षा के तीन अंग माने जाते हैं। शिक्षक, पाठ्यकम तथा बालक।।
9. शिक्षण संस्थाओं तक सीमित नहीं—सामान्य रूप से शिक्षण संस्थाओं अर्थात् स्कूल, कॉलेज में संपन्न होने वाली गतिविधियों को ही शिक्षा माना जाता है परंतु यह सत्य नहीं है। शिक्षा की। एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के समस्त क्षेत्रों से सम्बद्ध है।
शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य
शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं-
1. राष्ट्रीय विकास में योगदान-राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास में योगदान प्रदान करना है। वास्तव में, किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक होता है कि उसके अधिक-से-अधिक नागरिक शिक्षित हों। अधिकांश नागरिकों के अशिक्षित होने की स्थिति में कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति नहीं कर सकता। यह दो दृष्टिकोणों से सत्य है। सर्वप्रथम तो यह सत्य है कि अशिक्षित नागरिक राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में समुचित योगदान दे ही नहीं सकते। दूसरी बात यह सत्य है कि केवल शिक्षित व्यक्ति ही इस तथ्य को समझ पाते हैं कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति का महत्त्व अधिक होता है। शिक्षा द्वारा इस विवेक के विकास के परिणामस्वरूप राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होने लगता है|
![]()
2. राष्ट्रीय एकता के विकास में योगदान-राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक उल्लेखनीय कार्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखना भी है। हमारे देश के संदर्भ में शिक्षा का यह कार्य और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में बहुपक्षीय विविधता विद्यमान है। जातिगत, भाषागत, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधता हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक कारक हैं। इन कारकों के विद्यमान होने के कारण राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
3. भावात्मक एकता की वृद्धि–राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति के लिए भावात्मक एकता भी अति आवश्यक होती है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के रीति-रिवाज, प्रथाएँ, परंपराएँ तथा रहन-सहन में बहुत अधिक भिन्नता विद्यमान हैं। इस स्थिति में देश के विभिन्न भागों में नागरिकों में भावात्मक एकता को विकसित करने तथा बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास आवश्यक होते हैं। ये प्रयास शिक्षा के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है शिक्षा का एक मुख्य कार्य देश के नागरिकों में भावात्मक एकता में वृद्धि करना भी है।
4. सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का भाव विकसित करना—राष्ट्र के विकास, प्रगति एवं सुरक्षा आदि के लिए अनेक बार सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करनी भी आवश्यक होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक कार्य यह भी स्वीकार किया जाता है कि वह देश के नागरिकों में सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का भाव विकसित करे।।
5. योग्य कार्यकर्ता तैयार करना-राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य योग्य एवं निपुण कार्यकर्ता तैयार करना भी है। वास्तव में, योग्य एवं निपुण व्यक्ति ही राष्ट्रीय उन्नति एवं प्रगति में योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी कार्यों को उत्तम ढंग से करते हैं। औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अनुसंधान के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों द्वारा ही उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं। तथा राष्ट्र प्रगति करता है। इस प्रकार के योग्य एवं निपुण व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही तैयार होते हैं।
6. सामाजिक विकास का कार्य-राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक कार्य सामाजिकता का विकास करना भी है। इस गुण के विकास के परिणामस्वरूप समाज में अधिकांश व्यक्ति सामाजिक संघर्षों तथा तनावों से बचकर रहते हैं। सामाजिकता के गुण से युक्त नागरिक समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, वे अनावश्यक रूप से एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया करते।
7. सभ्यता तथा संस्कृति के सरंक्षण का कार्य किसी भी राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने तथा उसमें समुचित वृद्धि करने के लिए संबंधित सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण अति आवश्यक होता है। यह कार्य सर्वाधिक उत्तम रूप में शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। एकं प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ओटावे (Ottawey) के अनुसार, “शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों को उसके नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है।”
8. योग्य नागरिकों का निर्माण-न्यूयार्क की वैधानिक समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि “सार्वजनिक शैक्षिक व्यवस्था का एक प्रधान कार्य यह है कि वह विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों को निभाने योग्य बनाए।” वास्तव में, वही राष्ट्र उन्नति करता है जिसके अधिकांश नागरिक योग्य एवं नागरिकता के गुणों से युक्त होते हैं। शिक्षत्र का ही कार्य है कि वह लोगों को नागरिकता के गुणों की समुचित जानकारी प्रदान करे।
9. नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना-जनतांत्रिक देशों में कुशल नेतृत्व का भी विशेष महत्त्व होता है। जनतंत्र की सफलता के लिए योग्य, अनुभवी तथा कुशल नेताओं का होना अति आवश्यकता होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा का एक कार्य युवकों में नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है।
10. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का कार्य-आज प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय जीवन अतंर्राष्ट्रीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को पारस्परिक सहयोग से कार्य करने पड़ते हैं। अब विभिन्न राष्ट्र परस्पर पूरक रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के महत्त्व को स्वीकार किया जा चुका है। इस धारणा के विकास के साथ-ही-साथ शिक्षा का एक कार्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना भी मान लिया गया है। शिक्षा द्वारा विकसित की गई अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना ही विश्व-शान्ति तथा मैत्री को बढ़ावा दे सकती है तथा विश्व को युद्धों से बचाया जा सकता है।
पूर्वोक्त विवरण द्वारा शिक्षा के मुख्य कार्य स्पष्ट हो जाते हैं। वास्तव में शिक्षा के कार्य असंख्य हैं तथा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक पक्ष को उत्तम बनाना शिक्षा का ही कार्य है। राष्ट्र की प्रगति भी उत्तम शिक्ष पर ही निर्भर करती है।
![]()
सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका
आधुनिक समाजों में शिक्षा भी सामाजिक नियंत्रण का महत्त्वपूर्ण औपचारिक साधन है। इसे औपचारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्कूलों व कॉलेजों में औपचारिक विधि द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति समूह की मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त करता है तथा इससे इसे प्राप्त करने वालों के व्यवहार में नियमितता आती है। शिक्षा व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उसके चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांरित करने में भी सहायक है।
- सामाजिक व्यवहार का नियमन–शिक्षा मूल्यों, आदर्शों एवं मतों के संचार द्वारा व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है तथा इनसे उसका व्यवहार नियमित होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है तथा किस प्रकार को अनुचित। शिक्षा उचित व्यवहार की प्रेरणा देकर मानव के सामाजिक व्यवहार को नियमित करती है।
- व्यक्तित्व का विकास–औपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अच्छे गुण सीखता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इन गुणों व अच्छे व्यक्तित्व से वह अच्छा नागरिक बनता है और इस प्रकार वह स्वतः समाज के आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करता है। शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास का एक प्रमुख साधन माना गया है।
- आर्थिक सुरक्षा–शिक्षा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराकर भी सामाजिक नियंत्रण रखने में सहायक है। वस्तुतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से निर्भर बनाना, जीविकोपार्जन में सहायता देना तथा उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ाना है।
- अनुकूलन–शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान कर सामाजिक नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं का ज्ञान होता है तथा व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। इससे अनुकूलन’ में , सहायता मिलती है।
- संस्कृति का हस्तांतरण-शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में सहायता देकर भी सामाजिक नियंत्रण रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा द्वारा ही बच्चों को अपनी सामाजिक विरासत का ज्ञान प्राप्त होता है।
- भौतिक, बौद्धिक व नैतिक विकास–शिक्षा व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक व नैतिक विकास में सहायक है। इस बहुमुखी विकास द्वारा व्यक्ति तार्किक बन जाता है और समाज के आदर्शों के अनुरूप ही व्यवहार करता है।
- तनावों पर नियंत्रण शिक्षा व्यक्ति में अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहन देती है और तनावों पर नियंत्रण रखने में सहायक है। यह व्यक्तियों को नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करना सिखाती है। इससे भी सामाजिक नियंत्रण में इसका महत्त्व स्पष्ट होता है।
अतः शिक्षा सामाजिक नियंत्रण की एक महत्त्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है तथा बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक औपचारिक व अनौपचारिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करने में महत्त्वूपर्ण भूमिका निभाती है।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Sociology Introducing Sociology Chapter 3 Understanding Social Institutions (सामाजिक संस्थाओं को समझना) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Sociology Introducing Sociology Chapter 3 Understanding Social Institutions (सामाजिक संस्थाओं को समझना), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.