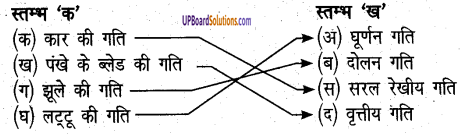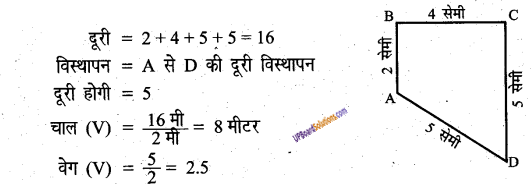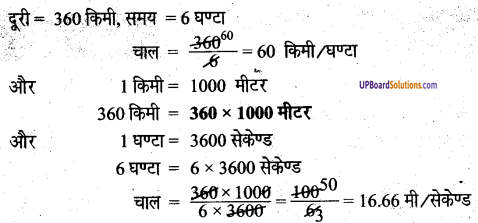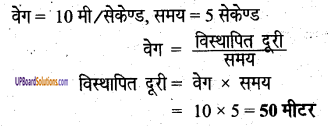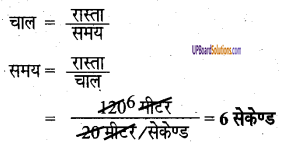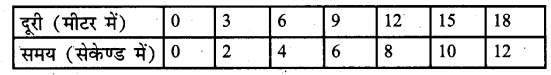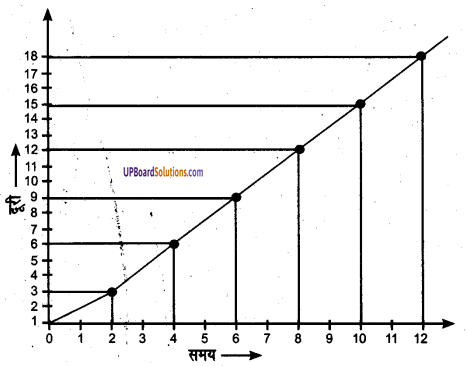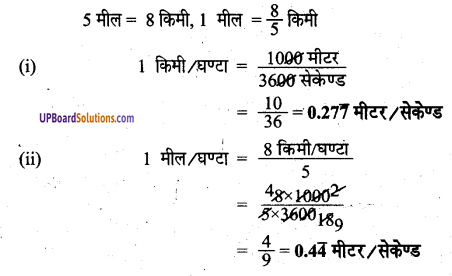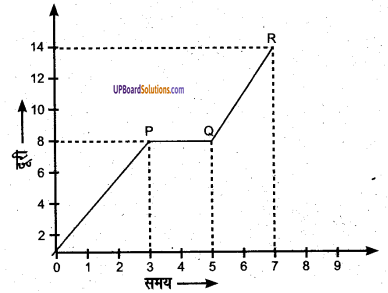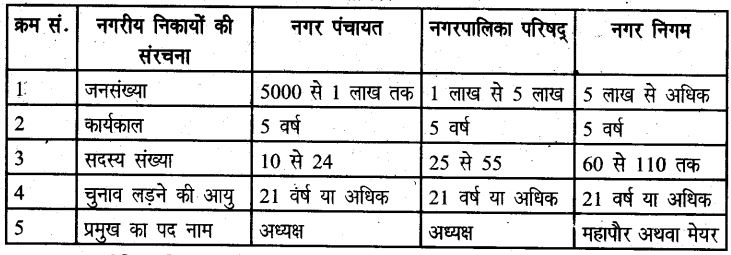UP Board Solutions for Class 6 Science Chapter 13 ऊर्जा
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 6 Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 6 Science Chapter 13 ऊर्जा.
ऊर्जा
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छाँटकर लिखिए –
(क) कोयले में होती है –
(i) ध्वनि ऊर्जा
(ii) रासायनिक ऊर्जा
(iii) विद्युत ऊर्जा
(iv) यांत्रिक ऊर्जा (✓)
![]()
(ख) गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा-
(i) रासायनिक ऊर्जा (✓)
(ii) ऊष्मीय ऊर्जा
(iii) यांत्रिक ऊर्जा
(iv) ध्वनि ऊर्जा
(ग) ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है-
(i) वायु (✓)
(ii) पत्थर का कोयला
(iii) जल
(iv) बायोमास
(घ) ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है|
(i) सौर ऊर्जा (✓)
(ii) लकड़ी
(iii) डीजल
(iv) पेट्रोल
![]()
प्रश्न 2.
निम्नलिखित सही कथनों के सामने (✓) व गलत के सामने (✗) का चिह्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए (लगाकर) –
उत्तर:
(क) किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। (✗)
(ख) जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। (✓)
(ग) ध्वनि ऊर्जा नहीं है। (✗)
(घ) बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है। (✓)
प्रश्न 3.
निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान अपनी अभ्यास-पुस्तिका में भरिए-
उत्तर:
(क) कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
(ख) चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में यांत्रिक ऊर्जा होती है।
(ग) पावर प्लांट द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है।
(घ) टार्च का सेल रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है।
प्रश्न 4.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिये-
(क) भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है?
उत्तर:
भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है।
![]()
(ख) कार्य का M.K.S व C.G.S मात्रक क्या है?
उत्तर:
कार्य का M.K.S.मात्रक जूल और C.G.S’ का मात्रक अर्ग है।
(ग) पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है?
उत्तर:
पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है।
(घ) कार्य और ऊर्जा में क्या सम्बन्ध है?
उत्तर:
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के – रूप में संचित हो जाता है।” जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती हैं। जिस (UPBoardSolutions.com) वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है, वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है।
![]()
प्रश्न 5.
ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं पाँच ईंधनों के नाम लिखें।
उत्तर:
ईंधन – ईंधन वे पदार्थ हैं, जिनको जलाने (दहन) से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे- लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम्।
प्रश्न 6.
गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्लांट द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं?
उत्तर:

गोबर गैस का नामांकित चित्रगोबर गैस द्वारा उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने तथा प्रकाश
उत्पन्न करने में किया जाता है।
● नौट – प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थी स्वयं करें।
We hope the UP Board Solutions for Class 6 Science Chapter 13 ऊर्जा help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 6 Science Chapter 13 ऊर्जा, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.