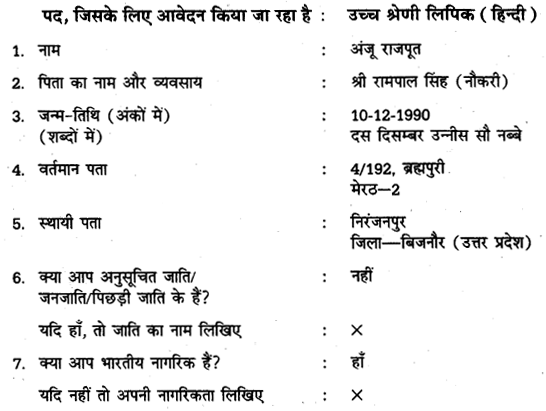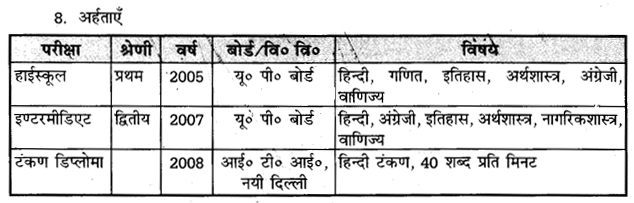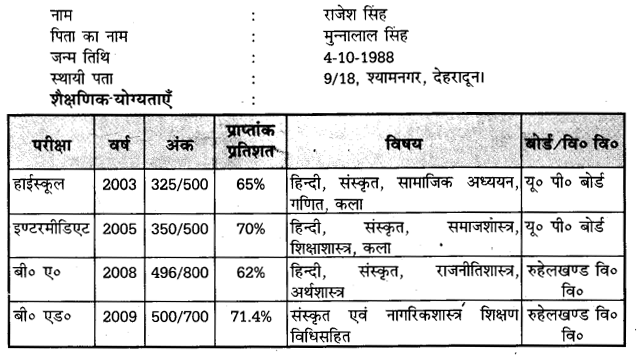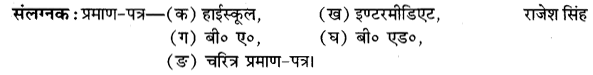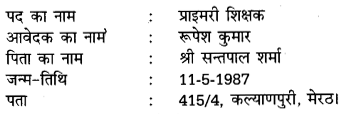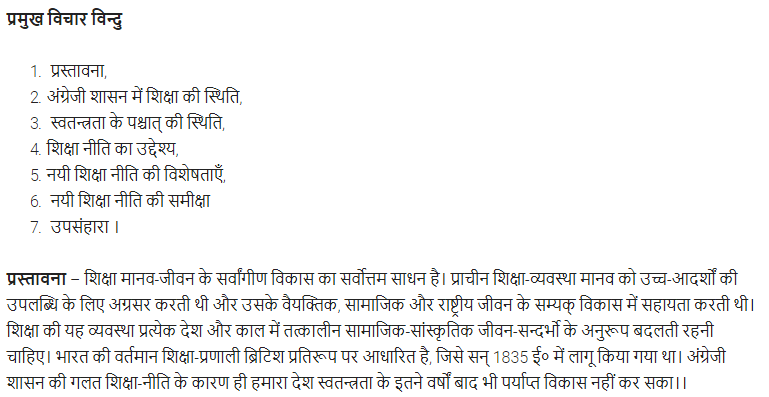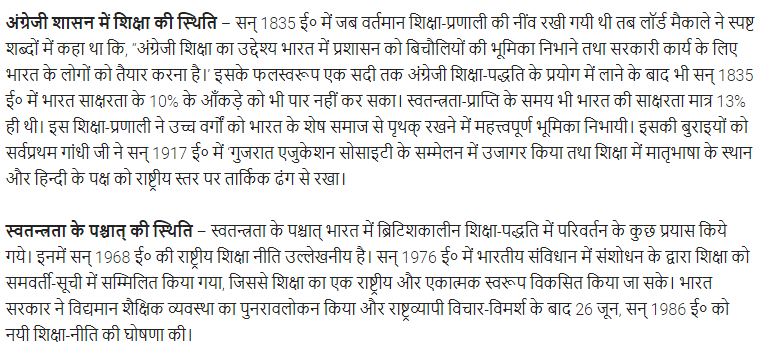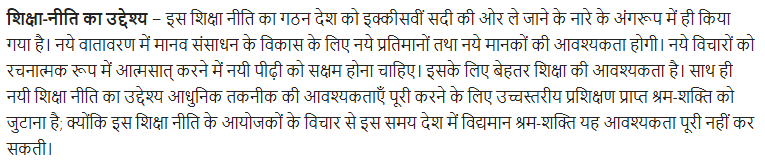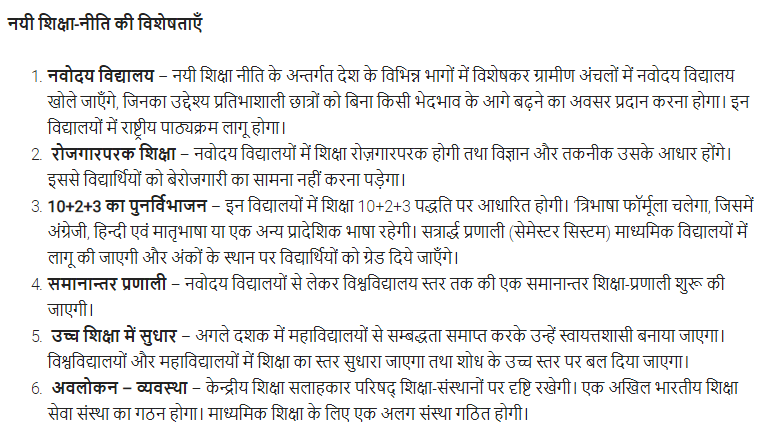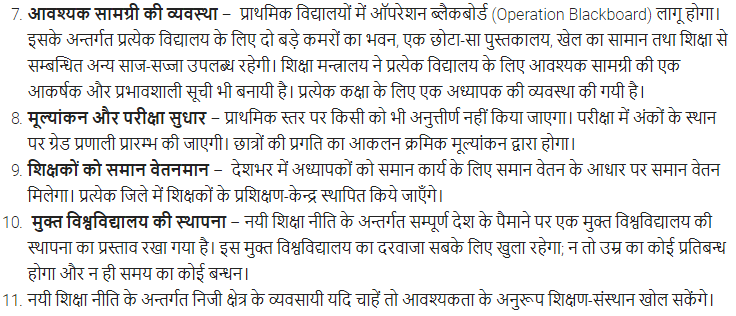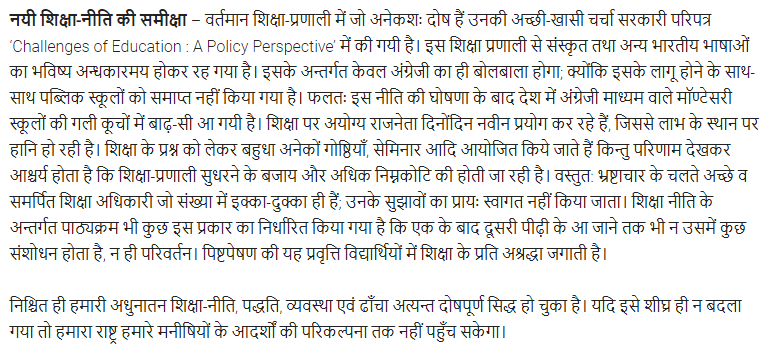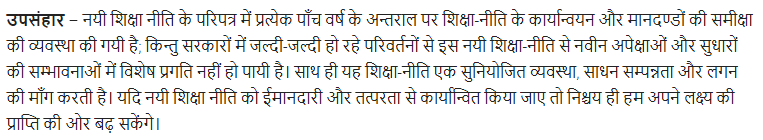UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 8 प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव are part of UP Board Solutions for Class 12 Home Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 8 प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव
| Board | UP Board |
| Class | Class 12 |
| Subject | Home Science |
| Chapter | Chapter 8 |
| Chapter Name | प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव |
| Number of Questions Solved | 33 |
| Category | UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 8 प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)
प्रश्न 1.
पर्यावरण कहते हैं
(a) प्रदूषण को
(b) वातावरण को
(c) पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर:
(c) पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को
प्रश्न 2.
वायु प्रदूषण के कारण हैं
(a) औद्योगीकरण
(b) वनों की अनियमित कटाई
(c) नगरीकरण
(d) ये सभी
उत्तर:
(d) ये सभी
प्रश्न 3.
जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन-से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
(a) सोडियम क्लोराइड
(b) कैल्शियम क्लोराइड
(C) ब्लीचिंग पाउडर
(d) पोटैशियम मेटाबाइसल्फाइट
उत्तर:
(c) ब्लीचिंग पाउडर
प्रश्न 4.
लाउडस्पीकर की आवाज से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है?
(a) वायु प्रदूषण
(b) ध्वनि प्रदूषण
(C) मृदा प्रदूषण
(d) जल प्रदूषण
उत्तर:
(b) ध्वनि प्रदूषण
प्रश्न 5.
ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं
(a) वाहनों के हॉर्न
(b) सायरन
(c) लाउडस्पीकर
(d) ये सभी
उत्तर:
(d) ये सभी
प्रश्न 6.
ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है
(a) आमाशय को
(b) वृक्क को
(c) कान को
(d) यकृत को
उत्तर:
(c) कान को
प्रश्न 7.
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 1 जून
(b) 5 जून
(c) 12 जून
(d) 18 जून
उत्तर:
(b) 5 जून
प्रश्न 8.
वस्तुओं के जलने से कौन-सी गैस बनती है?
(a) ऑक्सीजन
(b) कार्बन डाइऑक्साइड
(c) नाइट्रोजन
(d) अमोनिया
उत्तर:
(b) कार्बन डाइऑक्साइड
प्रश्न 9.
पर्यावरण रक्षा के लिए (2018)
(a) पेड़-पौधे उगाने चाहिए
(b) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना चाहिए
(c) नदियों को साफ रखना चाहिए।
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर:
(d) उपरोक्त सभी
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक, 25 शब्द)
प्रश्न 1.
पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए
उत्तर:
जिन्सबर्ट के अनुसार, “पर्यावरण वह सब कुछ है, जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।”
प्रश्न 2.
जनजीवन पर पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव को रोकने के बारे में लिखिए
उत्तर:
जनजीवन पर पर्यावरण का प्रमुख हानिकारक प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से पड़ता है। अतः पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करके उसके हानिकारक प्रभावों को रोका जा सकता है।
प्रश्न 3.
पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं?
उत्तर:
पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण | प्रदूषण कहलाता है।
प्रश्न 4.
पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? (2017)
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्न हैं।
- वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना।
- घरेलू अपमार्जकों का अधिकाधिक प्रयोग।
- वाहित मल का नदियों में गिरना।
- औद्योगिक अपशिष्ट तथा रासायनिक पदार्थों का विसर्जन।
प्रश्न 5.
प्रदूषण के प्रकार लिखिए। (2013)
उत्तर:
प्रदूषण के चार प्रकार हैं- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व मृदा प्रदूषण।
प्रश्न 6.
वायु प्रदूषण से होने वाली चार बीमारियों के नाम लिखिए। (2017)
अथवा
वायु प्रदूषण से फैलने वाले चार रोगों के नाम लिखिए। (2012)
उत्तर:
वायु प्रदूषण से चेचक, तपेदिक, खसरा, काली खाँसी आदि रोग हो जाते हैं।
प्रश्न 7.
वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं?
अथवा
पेड़-पौधे वातावरण को कैसे शुद्ध करते हैं?
उत्तर:
पेड़-पौधे वातावरण में ऑक्सीजन को विसर्जित करके उसे शुद्ध बनाए रखते हैं तथा वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं।
प्रश्न 8.
कल-कारखानों से वातावरण कैसेप्रदूषित होता है?
उत्तर:
कल-कारखानों से विसर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों (गन्दा जल, रसायन आदि) एवं गैसों (धुआँ) से जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, इसके अतिरिक्त इनमें उत्पन्न उच्च ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है।
प्रश्न 9.
जल प्रदूषण के कारण लिखिए।
अथवा
जल प्रदूषण के दो कारण लिखकर उनके निवारण के उपाय लिखिए।
उत्तर:
जल प्रदूषण के प्रमुख कारण जल स्रोतों में औद्योगिक अपशिष्टों एवं घरेलू वाहित मल का मिलना है। औद्योगिक अपशिष्ट को जल-स्रोतों में मिलने से रोकनी, सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, जैव उर्वरक के प्रयोग आदि से जल प्रदूषण का निवारण किया जा सकता है।
प्रश्न 10.
मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
मृदा प्रदूषण से जनजीवन पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं।
- मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव फसलों पर पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन घटता है।
- प्रदूषित मृदा में उत्पन्न भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न 11.
ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई क्या है?
उत्तर:
ध्वनि की तीव्रता के मापन की इकाई डेसीबल है।
प्रश्न 12.
ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए।
उत्तर:
सामान्यत: ध्वनि प्रदूषण के दो कारण होते हैं।
- प्राकृतिक
- कृत्रिम
लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक, 50 शब्द)
प्रश्न 1.
मानव जीवन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव लिखिए।
उत्तर:
वायु प्रदूषण मानव जीवन को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है।
- वायु प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं; जैसे—छाती एवं साँस सम्बन्धी बीमारियाँ-तपेदिक, फेफड़े का कैंसर आदि।
- वायु प्रदूषण से नगरों का वातावरण दूषित हो जाता है तथा अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण से बच्चों को खाँसी तथा साँस फूलने की समस्या पैदा होती है। वायु प्रदूषण महत्त्वपूर्ण स्मारकों, भवनों आदि के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाता है; जैसे-ताजमहल।।
- वायु प्रदूषण से वायुमण्डल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ती है, इससे ओजोन परत का क्षरण होता है।
- वायु प्रदूषण के कारण ओजोन क्षरण से पराबैंगनी किरणों का प्रभाव हमारे | ऊपर अधिक पड़ता है, जिससे त्वचा कैंसर जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो | सकती हैं।
- वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है।
- वायु प्रदूषण से कृषि एवं फसलों को नुकसान पहुँचता है। कृषि उत्पादन में कमी होती है। वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण बनता है, जिससे मानव, वनस्पति, भवन आदि सभी प्रभावित होते हैं।
प्रश्न 2.
संवातन किसे कहते हैं? यह क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
वायु प्राणियों के जीवन का एक आवश्यक तत्त्व है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु शुद्ध वायु आवश्यक है। संवातन से आशय ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें शुद्ध वायु का कमरे में प्रवेश और अशुद्ध वायु का निराकरण किया जाता है। अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तथा विभिन्न रोगों को निमन्त्रण देती है। संवातन हेतु घर में खिड़की, दरवाजों एवं रोशनदानों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे घर के अन्दर, बाहर से शुद्ध वायु का प्रवाह होता रहे एवं घर का वातावरण स्वस्थ बना रहे।
प्रश्न 3.
वायु प्रदूषण के कारण और रोकथाम के उपाय बताइए
अथवा
वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है?
उत्तर:
कुछ बाहरी कारकों के समावेश से किसी स्थान की वायु में गैसों के प्राकृतिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से धूलकण, धुआँ, कार्बन-कण, सल्फर डाइऑक्साइड (SO,), शीशी, कैडमियम आदि घातक पदार्थों के वायु में मिलने से होता है। ये सब उद्योग, परिवहन के साधनों, घरेलू भौतिक साधनों आदि के माध्यम से वायुमण्डल में मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है।
वायु प्रदूषण के कारण
वायु प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से फैलता है।
- औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न गैसे, धुआँ | आदि। विभिन्न प्रकार के ईंधनों; जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के दहन से उत्पन्न धुआँ एवं गैसें।
- वनों की अनियमित और अनियन्त्रित कटाई।
- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग।
वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय
वायु प्रदूषण को रोकने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं।
- पदार्थों का शोधन करना।
- घरेलू रसोई एवं उद्योगों आदि में ऊँची चिमनियों द्वारा धुएँ का निष्कासन।
- परिवहन के साधनों पर धुआँरहित यन्त्र लगाना।
- ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी, बायो डीजल आदि को प्रयोग करना।
प्रश्न 4.
जल प्रदूषण द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए
अथवा
जल प्रदूषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए
उत्तर:
जल प्रदूषण से मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं।
- प्रदूषित जल के सेवन से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं; जैसे-टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश।
- जल प्रदूषण से पेयजल का संकट उत्पन्न होता है।
- प्रदूषित जल वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं को हानि पहुँचाता है।
- प्रदूषित जल का कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- प्रदूषित जल के सेवन से दाँतों की समस्या, पेट की समस्या, कब्ज आदि | बीमारियाँ भी फैलती हैं। उदाहरण राजस्थान में प्रदूषित जल के सेवन से ‘नारू’ नामक रोग फैलने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
- मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है।
प्रश्न 5.
ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण में क्या अन्तर है?
उत्तर:

प्रश्न 6.
जल प्रदूषण के दो कारण लिखिए
उत्तर:
जल प्रदूषण के दो कारण निम्न प्रकार हैं।
- उद्योगों; जैसे-चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग आदि से निकलने वाला अपशिष्ट | पदार्थ, गन्दा जल आदि जल स्रोतों को दूषित कर देता है।
- नगरीकरण के परिणामस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों आदि का जल में मिलना। यमुना नदी इस प्रकार के प्रदूषण का ज्वलन्त उदाहरण है।
प्रश्न 7.
पर्यावरण प्रदूषण जनजीवन को कैसे प्रभावित करता है?
अथवा
व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में मानव के समक्ष उत्पन्न एक गम्भीर समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को हम निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं।
जन स्वास्थ्य पर प्रभाव
जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं।
- प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियाँ; जैसे-हैजा, कॉलरा, टायफाइड आदि होती हैं।
- ध्वनि प्रदूषण से सर दर्द, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप बढ़ना, उत्तेजना, हृदय की धड़कन बढ़ना आदि समस्याएँ होती हैं।
- जल प्रदूषण से टायफाइड, पेचिश, ब्लू बेबी सिण्ड्रोम, पाचन सम्बन्धी विकार (कब्ज) आदि समस्याएँ होती हैं।
- वायु प्रदूषण से फेफड़े एवं श्वास सम्बन्धी, श्वसन-तन्त्र की बीमारियाँ होती हैं। व्यक्तिगत कार्यक्षमता पर प्रभाव । व्यक्तिगत कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।
- इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता अनिवार्य रूप से घटती है।।
- प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता।
- प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति की चुस्ती, स्फूर्ति, चेतना आदि भी घट जाती है।
आर्थिक जीवन पर प्रभाव
आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण का गम्भीर प्रभाव जन सामान्य की आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक जीवन पर पड़ता है।
- कार्यक्षमता घटने से उत्पादन दर घटती है।
- साधारण एवं गम्भीर रोगों के उपचार में अधिक व्यय करना पड़ता है।
- आय दर घटने तथा व्यय बढ़ने पर आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पर बहुपक्षीय, गम्भीर तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। अत: इसके समाधान हेतु व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए।
प्रश्न 8.
पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है?
अथवा
पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए।
उत्तर:
पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनचेतना का होना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। सामान्य जनता को पर्यावरण के महत्त्व, भूमिका तथा प्रभाव आदिसे अवगत कराना आवश्यक है।
- वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए; जैसे-स्टॉकहोम सम्मेलन (1972), रियो डि जेनेरियो सम्मेलन (1992)।
- गाँव, शहर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र आदि सभी स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण में लोगों को शामिल करना चाहिए।
- पर्यावरण अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न सेमिनार पुनश्चर्या, कार्य-गोष्ठियाँ, | दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनी आदि का आयोजन कराया जा सकता है।
- विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर ‘पर्यावरण अध्ययन विषय को लागू करना एवं प्रौढ़ शिक्षा में भी पर्यावरण-शिक्षा को स्थान देना महत्त्वपूर्ण उपाय है।
- जनसंचार माध्यमों-रेडियो, दूरदर्शन तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
- पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना महत्त्वपूर्ण प्रयास है; जैसे-इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, इन्दिरा गाँधी पर्यावरण पुरस्कार आदि।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) का आयोजन जागरूकता लाने की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है।
प्रश्न 9.
मानव जीवन में जल का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
जल सभी जीवन-जन्तु एवं वनस्पतियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मानव के लिए तो ‘जल ही जीवन है ऐसा माना जाता है। जल का उपयोग केवल पीने के पानी और कृषि के लिए ही नहीं होता, बल्कि जल के अन्य कई उपयोग हैं; जैसे-कल-कारखानों और इण्डस्ट्रीज क्षेत्रों में भी जल अत्यन्त आवश्यक है। घर बनाने से लेकर मोटरगाड़ी इत्यादि चलाने, यातायात के साधनों तक सभी चीजों में ही जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में एक दिन पानी नहीं आता है, तो उस दिन उस घर का सारा काम बन्द हो जाता है; जैसे-खाना नहीं बन पाता, कपड़े नहीं धुल पाते, साफ-सफाई तथा स्नान आदि मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त जल की कमी के कारण कृषि सबसे अधिक प्रभावित होती है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे बाजार में उपलब्ध अनाजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। अतः जल मानव जीवन में हर क्षण महत्त्वपूर्ण है।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ( 5 अंक, 100 शब्द)
प्रश्न 1.
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण से आशय पर्यावरण के किसी एक या सभी भागों का दूषित होना है। यहाँ दूषित होने से आशय पर्यावरण के प्रकृति प्रदत्त रूप में इस प्रकार परिवर्तन होता है, जोकि मानव जीवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करे। पर्यावरण प्रदूषण जल, मृदा, वायु तथा ध्वनि के रूप में हो सकता है। पर्यावरण के इन कारकों के आधार पर ही पर्यावरण प्रदूषण के चार रूप हैं।
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
वायु प्रदूषण
कुछ बाहरी कारकों के समावेश से किसी स्थान की वायु में गैसों के प्राकृतिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से धूलकण, धुआँ, कार्बन-कण, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), शीशा, कैडमियम आदि घातक पदार्थों के वायु में मिलने से होता है। ये सब उद्योग, परिवहन के साधनों, घरेलू भौतिक साधनों आदि के माध्यम से वायुमण्डल में मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है।
जल प्रदूषण
जल के मुख्य स्रोतों में अशुद्धियों तथा हानिकारक तत्त्वों का समाविष्ट हो जाना ही जल प्रदूषण है। जल में जैव-रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायनों, सीसा, कैडमियम, बेरियम, पारा, फॉस्फेट आदि की मात्रा बढ़ने पर जल प्रदूषित हो जाता है। इन प्रदूषकों के कारण जल अपनी उपयोगिता खो देता है तथा जीवन के लिए घातक हो जाता है। जल प्रदूषण दो प्रकार का होता है-दृश्य प्रदूषण एवं अदृश्य प्रदूषण।।
मृदा प्रदूषण
मृदा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य रूप है। मिट्टी में पेड़-पौधों के लिए हानिकारक तत्त्वों का समावेश हो जाना ही मृदा प्रदूषण है।
मृदा प्रदूषण के कारण
मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित कारण होते हैं।
- मृदा प्रदूषण की दर को बढ़ाने में जल तथा वायु प्रदूषण का भी योगदान होता है।
- वायु में उपस्थित विषैली गैसे, वर्षा के जल में घुलकर भूमि पर पहुँचती हैं, जिससे मृदा प्रदूषित होती है।
- औद्योगिक संस्थानों से विसर्जित प्रदूषित जल तथा घरेलू अपमार्जकों आदि से युक्त जल भी मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है।
- इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूदीनाशकों आदि का अनियन्त्रित उपयोग भी मृदा को प्रदूषित करता है।
मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मृदा प्रदूषण, वायु एवं जल प्रदूषण से अन्तर्सम्बन्धित है। अतः इसकी रोकथाम के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में सतत् विकास को दृष्टि में रखते हुए, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का संयमित प्रयोग किया जाए।
ध्वनि प्रदूषण
ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का ही एक रूप है। पर्यावरण में अनावश्यक तथा अधिक शोर का व्याप्त होना ही ध्वनि प्रदूषण है। वर्तमान युग में शोर अर्थात् ध्वनि प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसको प्रतिकूल प्रभाव हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण की माप करने के लिए ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। इसकी माप की इकाई को डेसीबल कहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि 85 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि का पर्यावरण में व्याप्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः पर्यावरण में 85 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनियों का व्याप्त होना ध्वनि प्रदूषण है।
ध्वनि प्रदूषण के कारण
ध्वनि प्रदूषण के सामान्यत: दो कारण हैं
- प्राकृतिक
- कृत्रिम
प्राकृतिक कारण
- बादलों की गड़गड़ाहट
- बिजली की कड़के
- भूकम्प एवं ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि
- आँधी, तूफान आदि से उत्पन्न शोर।
कृत्रिम अथवा मानवीय कारण
ध्वनि प्रदूषण फैलाने में मुख्यतः कृत्रिम कारकों का ही महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
1.परिवहन के साधनों से उत्पन्न शोर जैसे बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, हवाई | जहाज, पानी का जहाज आदि से उत्पन्न ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं।
2.उद्योगों, फैक्टरियों आदि का शोर फैक्टरियों, औद्योगिक संस्थानों आदि की विशालकाय मशीनें, कलपुर्जे, इंजन आदि भयंकर शोर उत्पन्न करके ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं।
3.विभिन्न प्रकार के विस्फोट एवं सैनिक अभ्यास पहाड़ों को काटने की गतिविधियाँ एवं युद्ध क्षेत्र में गोला-बारूद आदि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण फैलता है।
4.मनोरंजन के साधन टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि मनोरंजन के साधन भी ध्वनि | प्रदूषण फैलाते हैं।
5.विभिन्न लड़ाकू एवं अन्तरिक्ष यान वायुयान, सुपरसोनिक विमान वे अन्तरिक्ष यान आदि ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं।
6.उत्सवों का आयोजन विभिन्न उत्सवों आदि में प्रयुक्त लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, डी. जे. आदि द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है।
शोर या ध्वनि प्रदूषण पर नियन्त्रण/उपचार
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रित करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं।
- उद्योगों के शोर के नियन्त्रण के लिए कारखाने आदि में शोर अवरोधक दीवारें तथा मशीनों के चारों ओर मफलरों का कवच लगाना चाहिए।
- कल-कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए।
- मोटर वाहनों में बहुध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
- उद्योगों में श्रमिकों को कर्ण प्लग या कर्ण बन्धकों का प्रयोग अनिवार्य किया | जाना चाहिए।
- आवास गृहों, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों, कार्यालयों आदि में उचित निर्माण सामग्री तथा उपयुक्त बनावट द्वारा शोर से बचाव किया जा सकता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अधिकतम शोर सीमा का निर्धारण करना चाहिए। ध्वनिरोधक सड़कों एवं भवनों को निर्माण करना अन्य उपाय हैं !
उपरोक्त उपायों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
प्रश्न 2.
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जल व वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने के उपाय लिखिए?
अथवा
जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कारण एवं इनकी रोकथाम के उपाय लिखिए।
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण से आशय पर्यावरण के किसी एक या सभी भागों का दूषित होना है। यहाँ दूषित होने से आशय पर्यावरण के प्रकृति प्रदत्त रूप में इस प्रकार परिवर्तन होता है, जोकि मानव जीवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करे। पर्यावरण प्रदूषण जल, मृदा, वायु तथा ध्वनि के रूप में हो सकता है। पर्यावरण के इन कारकों के आधार पर ही पर्यावरण प्रदूषण के चार रूप हैं।
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
वायु प्रदूषण
कुछ बाहरी कारकों के समावेश से किसी स्थान की वायु में गैसों के प्राकृतिक अनुपात में होने वाले परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से धूलकण, धुआँ, कार्बन-कण, सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), शीशा, कैडमियम आदि घातक पदार्थों के वायु में मिलने से होता है। ये सब उद्योग, परिवहन के साधनों, घरेलू भौतिक साधनों आदि के माध्यम से वायुमण्डल में मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है।
वायु प्रदूषण के कारण
वायु प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से फैलता है ।
- औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न गैसे, धुआँ आदि।
- विभिन्न प्रकार के ईंधनों; जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के | दहन से उत्पन्न धुआँ एवं गैसें।
- वनों की अनियमित और अनियन्त्रित कटाई।
- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग।
- घरेलू अपशिष्ट, खुले में शौच, कूड़ा-करकट इत्यादि।
- रसोईघर तथा कारखानों से निकलने वाला धुंआ।
- खनिजों का अवैज्ञानिक खनन एवं दोहन।
- विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों का विकिरण।
वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय
वायु प्रदूषण को रोकने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं।
- पदार्थों का शोधन करना।
- घरेलू रसोई एवं उद्योगों आदि में ऊँची चिमनियों द्वारा धुएँ का निष्कासन।
- परिवहन के साधनों पर धुआँरहित यन्त्र लगाना।
- ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी, बायो डीजल आदि का प्रयोग करना।
- वन तथा वृक्ष संरक्षण करना, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना।
- खुले में शौच न करना, बायोटायलेट का निर्माण करना।
- नगरों में मल-जल की निकासी का उचित प्रबन्ध करना।
- सीवर लाइन, टैंक आदि का निर्माण करना।
- नगरों में हरित पट्टी का विकास करना।
- प्रदूषण को रोकने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाना।
- स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बच्चों में चेतना फैलाना।
- उद्योगों, फैक्टरियों आदि को आवास स्थल से दूर स्थापित करना तथा उनसे निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण का समुचित उपाय करना।
जल प्रदूषण
जल के मुख्य स्रोतों में अशुद्धियों तथा हानिकारक तत्त्वों का समाविष्ट हो जाना ही जल प्रदूषण है। जल में जैव-रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायनों, सीसा, कैडमियम, बेरियम, पारा, फॉस्फेट आदि की मात्रा बढ़ने पर जल प्रदूषित हो जाता है। इन प्रदूषकों के कारण जल अपनी उपयोगिता खो देता है तथा जीवन के लिए घातक हो जाता है। जल प्रदूषण दो प्रकार का होता है-दृश्य प्रदूषण एवं अदृश्य प्रदूषण।।
जल प्रदूषण के कारण
जल प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से फैलता है।
- उद्योगों; जैसे-चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग आदि से निकलने वाला | अवशिष्ट पदार्थ, गन्दा जल आदि जल स्रोतों को दूषित कर देता है।
- नगरीकरण के परिणामस्वरूप अवशिष्ट पदार्थों आदि का जल में मिलना। यमुना नदी इस प्रकार के प्रदूषण का ज्वलन्त उदाहरण है।
- नदियों में कपड़े धोना अथवा उनमें नालों आदि का गन्दा जल मिलना।
- कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, अपमार्जकों आदि का वर्षा के माध्यम से जले स्रोतों में मिलना।
- समुद्री परिवहन, तेल का रिसाव आदि से जल स्रोत का दूषित होना।।
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन एवं खनन के परिणामस्वरूप विकिरण युक्त जल का नदी, समुद्र में पहुँचना।
- नदियों में अधजले शव, मृत शरीर आदि का विसर्जन।
- घरेलू पूजा सामग्री, मूर्तियों आदि का जल में विसर्जन।
जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय
जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय सम्भव हैं।
- नगरों में अशुद्ध जल को ट्रीटमेण्ट के उपरान्त शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ना।
- सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट एवं उद्योगों में ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाकर अशुद्ध जल एवं अवशिष्ट सामग्री का शोधन करना।।
- समुद्री जल में औद्योगिक गन्दगी आदि को न मिलने देना।
- मृत जीव एवं चिता के अवशेष आदि नदियों में प्रवाहित न होने देना।
- नदियों तथा तालाबों की समय-समय पर सफाई करना।
- नदियों, तालाबों के जल में कपड़े न धोना।
- नदियों में धार्मिक आयोजन के अवशिष्ट पदार्थों को न फेंकना।
- कृषि में जैव उर्वरकों को प्रयोग करना।।
- जल प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जन-जागरूकता फैलाना एवं सहयोग के लिए प्रेरित करना
प्रश्न 3.
पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण बताइए?
अथवा
पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारकों का उल्लेख कीजिए तथा उसे नियन्त्रित करने के उपाय भी बताइए।
अथवा
पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण तथा मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
पर्यावरण प्रदूषण से आशय
पर्यावरण प्रदूषण से आशय पर्यावरण के किसी एक या सभी भागों का दूषित होना है। यहाँ दूषित होने से आशय पर्यावरण के प्रकृति प्रदत्त रूप में इस प्रकार परिवर्तन होता है, जोकि मानव जीवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करे। पर्यावरण प्रदूषण जल, मृदा, वायु तथा ध्वनि के रूप में हो सकता है। पर्यावरण के इन कारकों के आधार पर ही पर्यावरण प्रदूषण के चार रूप हैं।
- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण
पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गम्भीर तथा व्यापक समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः मानव समाज ही जिम्मेदार है। विश्व में मानव ने जैसे-जैसे सभ्यता का बहुपक्षीय विकास किया है, वैसे-वैसे उसने प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया है। पर्यावरण प्रदूषण के असंख्य कारण हैं, परन्तु उनमें से मुख्य एवं अधिक प्रभावशाली सामान्य कारण निम्नलिखित हैं।
1.औद्योगीकरण तीव्र औद्योगीकरण पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक मुख्य कारक है। औद्योगिक संस्थानों में ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है, वहीं औद्योगिक अपशिष्टों का उत्सर्जन जल एवं मृदा प्रदूषण तथा उद्योगों की मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण फैलाने में सहायक है। विश्व में हर जगह तीव्र औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।
2.नगरीकरण नगरीकरण के परिणामस्वरूप जनसंख्या के बड़े भाग का नगरीय क्षेत्रों में बसना प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना, पानी की अतिरेक खपत, परिवहन साधनों के बढ़ते प्रयोग आदि ने प्रदूषण बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
3.घरेलू जल-मल का अनियमित निष्कासन आवासीय क्षेत्रों में खुले में शौच, विभिन्न घरेलू अपशिष्ट आदि द्वारा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है।
4.घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग घर में प्रयुक्त अनेक अपमार्जक पदार्थ; जैसे-मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच, दीमक आदि को नष्ट करने के लिए विभिन्न दवाओं का प्रयोग, विभिन्न दवाइयाँ एवं साबुन, तेल आदि वायु अथवा जल के माध्यम से हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करते हैं।
5.दहन एवं धुआँ रसोईघर, उद्योगों, परिवहन के साधनों आदि द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसों एवं धुएँ में वृद्धि से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जोकि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है।।
6.कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कृषि कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। विभिन्न लाभकारक कीटों को भी कीटनाशकों द्वारा समाप्त किया जाता है। कीटनाशक एवं उर्वरक वर्षा जल के माध्यम से नदियों में मिलकर एवं नृदा में मिलकर जल एवं मृदा प्रदूषण में योगदान करते हैं फीनोल, मेथाक्सीक्लोर आदि कीटनाशकों एवं उर्वरक के प्रमुख उदाहरण हैं।
7.वृक्षों की अत्यधिक कटाई/वन विनाश वन विनाश के परिणामस्वरूप वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि वन/वृक्ष ही जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर एवं प्राणदायक ऑक्सीजन प्रदान करके वायुमण्डल में ऑक्सीजन का सन्तुलन बनाए रखते हैं। अत: वन विनाश पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है।
8.विभिन्न भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि वर्तमान समय में प्रयुक्त | एसी, फ्रिज, वाटरहीटर आदि से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसे निकलती हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है। एसी से निकलने वाली सीएफसी गैस इसका प्रमुख उदाहरण है।
9.परिवहन के साधन वर्तमान समय में परिवहन के साधनों; जैसे-कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इन साधनों में पेट्रोल डीजल के दहन से विभिन्न जहरीली गैसें; जैसे-कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि निकलती हैं, जिनसे वायु प्रदूषण होता है। इनके चलने से एवं हॉर्न से उत्पन्न शोर से क्रमशः ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।
10.रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा प्रदूषण परमाणु ऊर्जा, परमाणु परीक्षणों आदि से वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का समावेश होता है, जोकि पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। इस कारक का पर्यावरण के जीव-जन्तुओं तथा वनस्पति पर हानिकर प्रभाव पड़ता है।
पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम/ नियन्त्रण के उपाय
पर्यावरण प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है। वर्तमान समय में विश्व के समस्त देश इस समस्या को लेकर चिन्तित हैं तथा इसके समाधान हेतु प्रयासरत् हैं। भारत एवं विश्व में इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं।
- उद्योगों एवं घरेलू स्तर पर धुएँ की निकासी हेतु ऊँची चिमनी का प्रयोग – करना।
- उद्योगों एवं फैक्टरियों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, जल आदि को पूर्ण | रूप से उपचारित करने के पश्चात् ही निष्कासित करना।
- फैक्टरियों एवं उद्योगों की स्थापना आवासीय क्षेत्र से दूर करना।
- वाहन प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों की समय-समय पर जाँच | करवाना।
- ईंधन की कम-से-कम खपत करना, अनावश्यक ईंधन व्यर्थ न करना।
- कृषि में जैव-उर्वरकों का प्रयोग करना। परिवहन ईंधन के रूप में सीएनजी, एलपीजी आदि पर्यावरण हितैषी ईंधन को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन हेतु एलपीजी एवं गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना करना।
- जन सामान्य को पर्यावरण के प्रति सचेत करना। | इन सभी उपायों को लागू करके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
जन स्वास्थ्य पर प्रभाव
जन स्वास्थ्य पर प्रभाव निम्नलिखित हैं।
- प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियाँ; जैसे-हैजा, कॉलरा, टायफाइड आदि होती हैं।
- ध्वनि प्रदूषण से सर दर्द, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप बढ़ना, उत्तेजना, हृदय की धड़कन बढ़ना आदि समस्याएँ होती हैं।
- जल प्रदूषण से टायफाइड, पेचिश, ब्लू बेबी सिण्ड्रोम, पाचन सम्बन्धी विकार (कब्ज) आदि समस्याएँ होती हैं।
- वायु प्रदूषण से फेफड़े एवं श्वास सम्बन्धी, श्वसन-तन्त्र की बीमारियाँ होती हैं।
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 8 प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Home Science Chapter 8 प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.