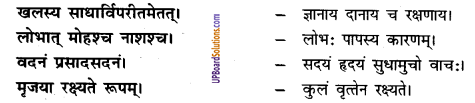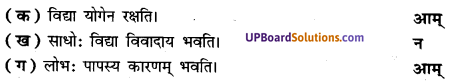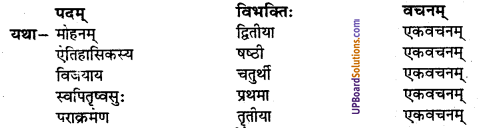UP Board Solutions for Class 10 Hindi गद्य-साहित्य के विकास पर आधारित
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Hindi गद्य-साहित्य के विकास पर आधारित.
हिन्दी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय
विशेष-पाठ्यक्रम के नवीनतम प्रारूप के अनुसार हिन्दी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय’ के अन्तर्गत केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर युग (छायावादोत्तर युग) ही निर्धारित हैं, किन्तु अध्ययन की दृष्टि से यहाँ सभी युगों के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों को संक्षेप में दिया जा रहा है, क्योंकि एक-दूसरे से घनिष्ठता के कारण कभी-कभी निर्धारित युग से अलग प्रश्न भी पूछ लिये जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, केवल विस्तृत अध्ययन के लिए दिये गये हैं। इससे प्रायः अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
गद्य-साहित्य के विकास पर आधारित
प्रश्न 1
गद्य का अर्थ लिखिए।
उत्तर
गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का (UPBoardSolutions.com) नाम है। इसकी विषय-वस्तु हमारी बोध-वृत्ति पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति या भावना होती है। गद्य वास्तविकता और व्यावहारिकता से ओत-प्रोत होता है।
प्रश्न 2
गद्य और पद्य (काव्य) में अन्तर बताइट।
उत्तर
गद्य मस्तिष्क के तर्कप्रधान चिन्तन की उपज होता है और छन्दबद्ध, भावपूर्ण तथा ओजयुक्त रचनाएँ काव्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यावहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत-रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है।

प्रश्न 3
गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है ?
उत्तर
गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोल-चाल की भाषा के रूप में होता है।
प्रश्न 4
भाषा-रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियाँ उपलब्ध हैं ?
उत्तर
भाषा-रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की चार कोटियाँ–
- वर्णनात्मक,
- विवेचनात्मक,
- भावात्मक,
- विवरणात्मक उपलब्ध हैं।
प्रश्न 5
सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक-एक विधा का नाम लिखिए।
उत्तर
- सृजनात्मक गद्य-विधा–निबन्ध तथा
- उपयोगी गद्य-विधा–विज्ञानपरक लेखन।

प्रश्न 6
गद्य का महत्त्व समझाइए।
उत्तर
गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज (UPBoardSolutions.com) भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान-विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है।
प्रश्न 7
हिन्दी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ ?
उत्तर
हिन्दी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ।
प्रश्न 8
हिन्दी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं ?
उत्तर
हिन्दी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और (UPBoardSolutions.com) ब्रजभाषा में मिलते हैं।

प्रश्न 9
प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है ?
या
राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है ?
उत्तर
राजस्थानी गद्य हमें दसवीं शताब्दी के दानपत्रों, पट्टे-परवानों, टीकाओं व अनुवाद-ग्रन्थों के रूप में देखने को मिलता है।
प्रश्न 10
ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आस-पास हुआ ?
उत्तर
ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत् 1400 वि० (UPBoardSolutions.com) (सन् 1343 ई०) के आस-पास हुआ।
प्रश्न 11
ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए।
या
ब्रजभाषा गद्य के दो प्रमुख लेखक तथा उनकी एक-एक रचना का नाम लिखिए।
उत्तर
- गोस्वामी बिट्ठलनाथ, रचना–‘श्रृंगार रस-मण्डन’।
- गोकुलनाथ, रचना–‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ और ‘दो सौ बावन वैष्णवन की। वार्ता।
प्रश्न 12
खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रन्थ में होते हैं ?
या
खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उसकी प्रथम रचना का नाम लिखिए।
उत्तर
खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित (UPBoardSolutions.com) ‘चंद छंद बरनन की महिमा’ नामक ग्रन्थ में होते हैं।

अत: कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना ‘चंद छंद बरनन की महिमा’ को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाना चाहिए। कुछ विद्वान जटमलकृत ‘गोरा बादल की कथा’ को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं।
प्रश्न 13
कवि गंग किसके दरबारी कवि थे ?
उत्तर
कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे।
प्रश्न 14
भारतेन्दु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम चार उन्नायकों के नाम, उनकी एक-एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचनाकाल बताइए।
उत्तर
भारतेन्दु युग से पूर्व खड़ी बोली हिन्दी गद्य के प्रारम्भिक (UPBoardSolutions.com) चार उन्नायकों के नाम और उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं-
- मुंशी इंशा अल्ला खाँ–‘रानी केतकी की कहानी’,
- सदासुखलाल– ‘सुखसागर’,
- सदल मिश्र-‘नासिकेतोपाख्यान’,
- लल्लूलाल-‘प्रेमसागर’। इन सभी कृतियों का रचनाकाल सन् 1803 ई० के आस-पास है।

प्रश्न 15
सदल मिश्र और इंशा अल्ला खाँ की शैली का अन्तर बताइए।
उत्तर
सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए हैं, जबकि इंशा अल्ला खाँ की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं।
प्रश्न 16
लल्लूलाल और इंशा अल्ला खाँ की भाषा में क्या मुख्य अन्तर है ?
उत्तर
लल्लूलाल की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव है, जबकि इंशा अल्ला खाँ की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी, संस्कृत तथा ब्रजभाषा के शब्द नहीं हैं।
प्रश्न 17
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को ‘रंगीन और चुलबुली’ कहा है ?
उत्तर
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इंशा अल्ला खाँ की भाषा (UPBoardSolutions.com) को रंगीन और चुलबुली’ कहा है।

प्रश्न 18
आर्य समाज का हिन्दी गद्य के विकास में क्या योगदान है ?
उत्तर
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार हिन्दी भाषा में किया तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ की रचना भी हिन्दी भाषा में ही की। वेदों के भाष्य भी उन्होंने हिन्दी भाषा में ही लिखे तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिन्दी गद्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।
प्रश्न 19
हिन्दी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा है।
उत्तर
ईसाई पादरियों ने अपने धर्म-प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिन्दी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ-साथ हिन्दी भाषा के (UPBoardSolutions.com) गद्य का प्रचार-प्रसार भी होता रहा।

प्रश्न 20
भारतेन्द्र से पूर्व कौन-से दो राजाओं ने हिन्दी गद्य के विकास में योगदान दिया ?
या
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द’ तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा-शैली का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
भारतेन्दु से पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द’ ने अरबी-फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली को अपनाया। इन दोनों की भाषा-शैली का यही मुख्य अन्तर है।
प्रश्न 21
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द’ की भाषा के क्या दोष थे ?
उत्तर
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द’ की भाषा पर अरबी-फारसी का प्रभाव था। इसी को उनकी खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है।
प्रश्न 22
राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था ?
उत्तर
राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृतनिष्ठ थी। ये दैनिक प्रयोग में (UPBoardSolutions.com) काम आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के सामान्य शब्दों को भी हिन्दी से दूर रखना चाहते थे।

प्रश्न 23
बीसवीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिन्दी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किये ?
उत्तर
बीसवीं शताब्दी में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किये।।
प्रश्न 24
हिन्दी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरम्भ हुआ ?
या
गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ ? (2016)
उत्तर
हिन्दी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेन्दुकोल–सन् 1850 ई०-से आरम्भ हुआ।
प्रश्न 25
भारतेन्दु युग में किन गद्य-विधाओं का विकास हुआ ?
उत्तर
भारतेन्दु युग में नाटक, निबन्ध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य-विधाओं का विकास
हुआ।
प्रश्न 26
भारतेन्दु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए।
उत्तर
संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों (UPBoardSolutions.com) तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेन्दु युग की भाषा में सजीवता आ गयी थी।

प्रश्न 27
भारतेन्दु युग का काल-निर्धारण कीजिए।
उत्तर
हिन्दी गद्य के विकास में सन् 1850 से 1900 ई० तक का समय भारतेन्दु युग कहलाता है।
प्रश्न 28
आधुनिक हिन्दी-निर्माताओं की वृहत्-त्रयी में किन लेखकों को गिना जाता है ?
उत्तर
आधुनिक हिन्दी-निर्माताओं की वृहत्-त्रयी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र की गणना की जाती है।
प्रश्न 29
भारतेन्दु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
भारतेन्दु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं
- इस युग में हिन्दी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ तथा ।
- इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहरी समर्पण-भावना थी।
प्रश्न 30
भारतेन्दु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। |
या
उन्नीसवीं शताब्दी के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए।
या
भारतेन्दु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए।
या
भारतेन्दु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। (2015)
उत्तर
भारतेन्दु युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेन्दु के अतिरिक्त (UPBoardSolutions.com) श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, कार्तिकप्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बदरीनारायण चौधरी, ‘प्रेमघन’ के नाम प्रमुख हैं।।

प्रश्न 31
द्विवेदी युग में गद्य के किन-किन रूपों का विकास हुआ ?
उत्तर
द्विवेदी युग में गद्य के रूपों; निबन्ध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक; का विकास हुआ।
प्रश्न 32
द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
- भाषा संस्कार तथा
- गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास; द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएँ हैं।
प्रश्न 33
हिन्दी-साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर
हिन्दी-साहित्य का प्रचारे और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम निम्नवत् हैं
- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी और
- हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।

प्रश्न 34
उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द का उत्तराधिकार जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया, उनमें से दो लेखकों के नाम लिखिए।
उत्तर
उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द का उत्तराधिकार वहन करने वाले लेखक
- जैनेन्द्र कुमार और
- आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं।
प्रश्न 35
द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए।
या
द्विवेदी युग के दो महत्त्वपूर्ण लेखकों के नाम लिखिए। [2009]
उत्तर
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्णसिंह, पद्मसिंह शर्मा, श्यामसुन्दर दास तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक अथवा साहित्यकार हैं।
प्रश्न 36
द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों अथवा साहित्य-इतिहास लेखकों के नाम लिखिए।
उत्तर
द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों अथवा साहित्य-इतिहास लेखकों के नाम इस प्रकार हैं–
- पद्मसिंह शर्मा,
- श्यामसुन्दर दास तथा
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल।
प्रश्न 37
हिन्दी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए।
या
किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। [2014]
उत्तर
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं।
प्रश्न 38
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं ?
उत्तर
श्री बख्शी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं।
प्रश्न 39
हिन्दी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है ?
उत्तर
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों (UPBoardSolutions.com) के प्रकाशन से हिन्दी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है।
प्रश्न 40
आलोचना द्वारा गद्य-साहित्य को नयी दिशा किस लेखक ने प्रदान की ?
उत्तर
आलोचना द्वारा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने गद्य-साहित्य को एक नयी दिशा प्रदान की।

प्रश्न 41
द्विवेदी युग की कालावधि लिखिए।
उत्तर
द्विवेदी युग की कालावधि सन् 1900 से 1920 ई० तक है। कालावधि का यह निर्धारण ‘सरस्वती’ पत्रिका की प्रमुखता के आधार पर किया गया है।
प्रश्न 42
आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी किस विधा-लेखन के लिए जाने जाते हैं ?
उत्तर
आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी निबन्ध और इतिहास-लेखन के लिए जाने जाते हैं।
प्रश्न 43
शुक्ल जी की भाषा-शैली की दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर
- शुक्ल जी की भाषा-शैली गठी हुई है, जिसमें शब्दों के साथ-साथ वाक्य भी गुंथे रहते हैं।
- शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है।
प्रश्न 44
रामचन्द्र शुक्ल की गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है ?
या
रामचन्द्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है ?
उत्तर
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की
- आलोचना और
- निबन्ध नामक गद्य की दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है और इन्हीं दो विधाओं के लेखन में उन्हें सर्वाधिक सफलता भी मिली है।
प्रश्न 45
रामचन्द्र शुक्ल के दो आलोचना-ग्रन्थों के नाम लिखिए।
उत्तर
- रस-मीमांसा और
- चिन्तामणि; रामचन्द्र शुक्ल के दो आलोचना-ग्रन्थ हैं।
प्रश्न 46
शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी-लेखकों के नाम लिखिए।
या
शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। [2013]
उत्तर
शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी-लेखक हैं—
- भगवतीचरण वर्मा तथा
- आचार्य चतुरसेन शास्त्री।
प्रश्न 47
शुक्ल युग के दो प्रमुख हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए।
या
शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। [2010, 15]
या
शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहास-लेखकों के नाम लिखिए।
या
शुक्ल पक्ष के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबन्धकारों के नाम लिखिए।
या
शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबन्धकार का नाम लिखिए। [2012]
उत्तर
शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक निम्नवत् हैं-
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा
- बाबू गुलाबराय इतिहासकार/निबन्धकार हैं।

प्रश्न 48
शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए।
या
शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए।
या
शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए।
उत्तर
(1) डॉ० नगेन्द्र; कृतियाँ–
- विचार और अनुभूति,
- अनुसन्धान और आलोचना,
- आस्था के चरण,
- अप्रवासी की यात्राएँ आदि।
(2) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी; कृतियाँ-
- अशोक के फूल,
- कुटज,
- विचार-प्रवाह,
- पुनर्नवा आदि।
प्रश्न 49
शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो प्रमुख हिन्दी आलोचकों के नाम लिखिए। [2011, 14]
उत्तर
शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख हिन्दी आलोचकों के नाम निम्नवत् हैं
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा
- पं० नन्ददुलारे वाजपेयी।
प्रश्न 50
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बाद के किन्हीं दो साहित्य-इतिहास लेखकों के नाम लिखिए।
या
आलोचना और इतिहास-लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बाद किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया ? उनके नाम बताइए।
उत्तर:
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पश्चात् (शुक्लोत्तर युग) आलोचना (UPBoardSolutions.com) और इतिहास-लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों के नाम हैं-आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० रामकुमार वर्मा आदि।।

प्रश्न 51
शुक्लोत्तर युग की समय-सीमा बताइट। [2012, 13]
उत्तर
शुक्ल युग के पश्चात् यानि सन् 1938 से सन् 1980 के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है।
प्रश्न 52
हिन्दी-साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए।
या
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। [2012]
उत्तर
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,
- श्यामसुन्दर दास तथा
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न 53
प्रेमचन्द के समकालीन किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए।
उत्तर
प्रेमचन्द के समकालीन दो लेखकों के नाम हैं—
- श्री जयशंकर प्रसाद तथा
- श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला’।
प्रश्न 54
छायावादी युग के गद्य-साहित्य की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
छायावादी युग के गद्य-साहित्य की विशेषताएँ हैं-
- प्रतीकात्मकता,
- लाक्षणिकता,
- आलंकारिकता एवं
- वक्रता।
प्रश्न 55
छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए।
या
किन्हीं दो छायावादी लेखकों तथा उनकी एक-एक रचना का नाम लिखिए। [2009, 12]
उत्तर
- जयशंकर प्रसाद-चन्द्रगुप्त तथा
- महादेवी वर्मा-स्मृति की रेखाएँ।
प्रश्न 56
छायावादोत्तर युग के किसी एक प्रमुख कवि और गद्य लेखक का नाम लिखिए। उसकी एक काव्य तथा एक गद्य-रचना का नाम भी लिखिए।
उत्तर
लेखक-रामधारी सिंह ‘दिनकर’। काव्य-रचना–कुरुक्षेत्र, (UPBoardSolutions.com) गद्य-रचना-अर्द्धनारीश्वर।

प्रश्न 57
शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख विशेषताएँ संक्षेप में लिखिए।
या
शुक्लोत्तर युग के साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
- शुक्लोत्तर युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है।
- शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यावहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशीलता और विषय-वैविध्य से ओत-प्रोत है।
प्रश्न 58
उस लेखिका का नाम बताइए, जिसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी किन्हीं दो गद्य-रचनाओं के नाम निर्दिष्ट कीजिए।
उत्तर
छायावादी युग की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी दो गद्य रचनाएँ हैं—
- पथ के साथी तथा
- स्मृति की रेखाएँ।
प्रश्न 59
प्रगतिवादी युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइट।
उत्तर
- प्रगतिवादी युग में सहज, व्यावहारिक और अलंकारविहीन गद्य की रचना हुई।
- प्रगतिवादी युग में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का (UPBoardSolutions.com) स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों से युक्त रचनाओं ने ले लिया।
प्रश्न 60
हिन्दी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम लिखिए।
या
प्रगतिवादी युग के लेखकों में से किसी एक लेखक का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर
हिन्दी के दो प्रगतिवादी लेखक हैं—
- डॉ० रामविलास शर्मा तथा
- शिवदानसिंह चौहान।
प्रश्न 61
प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो साहित्यिक रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए।
उत्तर
प्रगतिवादी युग में लिखी गयी दो साहित्यिक रचनाओं के नाम हैं—
- रतिनाथ की चाची (लेखक : वैद्यनाथ मिश्र, प्रसिद्ध नाम नागार्जुन) तथा
- मैला आँचल (लेखक : फणीश्वर नाथ ‘रेणु’)।
प्रश्न 62
हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा विनयमोहन शर्मा किस काल के लेखक थे ?
उत्तर
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा विनयमोहन (UPBoardSolutions.com) शर्मा छायावादोत्तर काल के लेखक थे।

प्रश्न 63
हिन्दी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताइट।
या
हिन्दी गद्य की किन्हीं चार विधाओं के नाम लिखिए।
या
हिन्दी गद्य की किन्हीं दो विधाओं के नाम लिखिए। [2009, 10]
उत्तर
हिन्दी गद्य की प्रमुख विधाएँ हैं-निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा आलोचना।
प्रश्न 64
हिन्दी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखिए।
उत्तर
हिन्दी गद्य की दो नवीन विधाएँ हैं—
- डायरी तथा
- रिपोर्ताज।
प्रश्न 65
हिन्दी गद्यकाव्य-लेखकों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए।
उत्तर
- वियोगी हरि तथा
- रायकृष्ण दास; हिन्दी के दो गद्यकाव्य लेखक हैं।
प्रश्न 66
‘रानी केवकी की कहानी’ और ‘कलम का सिपाही’ के लेखकों के नाम लिखिए।
या
‘कलम का सिपाही’ नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए। [2011]
उत्तर
‘रानी केतकी की कहानी’ के लेखक मुंशी इंशा अल्ला (UPBoardSolutions.com) खाँ व ‘कलम का सिपाही’ के लेखक अमृतराये हैं।

प्रश्न 67
हिन्दी गद्य की किन्हीं चार प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर
- निबन्ध–श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारीप्रसाद द्विवेदी।
- नाटक–जयशंकर प्रसाद, वृन्दावनलाल वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क’, मोहन राकेश।
- कहानी-प्रेमचन्द, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद।।
- उपन्यास-प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री।
प्रश्न 68
हिन्दी के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए।
या
हिन्दी के दो महाकाव्यों और उनके लेखकों के नाम लिखिए।
उत्तर
हिन्दी के दो महाकाव्यों के नाम हैं-
- श्रीरामचरितमानस और
- कामायनी।
इनके लेखकों के नाम हैं—
- गोस्वामी तुलसीदास तथा
- श्री जयशंकर प्रसाद।
प्रश्न 69
‘आवारा मसीहा’ किस विधा की रचना है? [2016]
उत्तर
जीवनी।।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Hindi गद्य-साहित्य के विकास पर आधारित help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Hindi गद्य-साहित्य के विकास पर आधारित, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
![]()
![]()
![]()