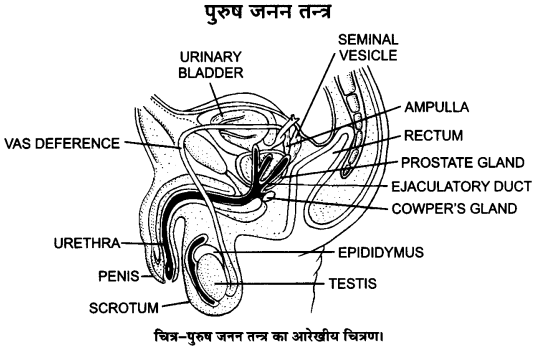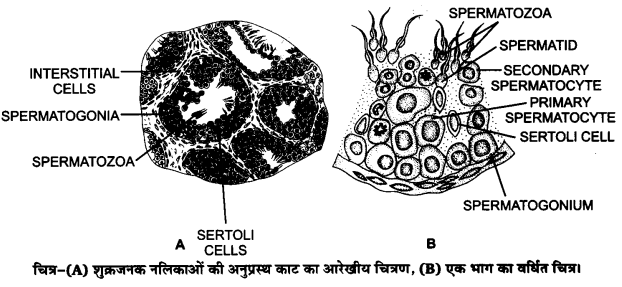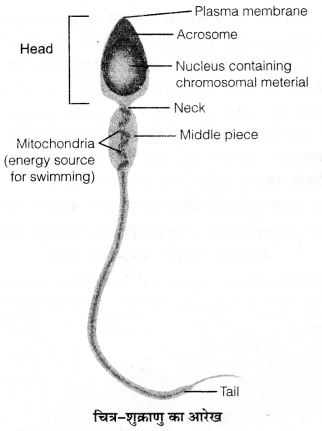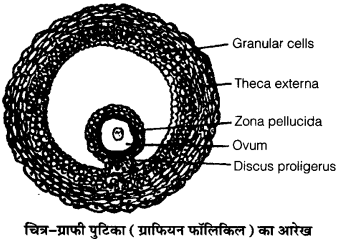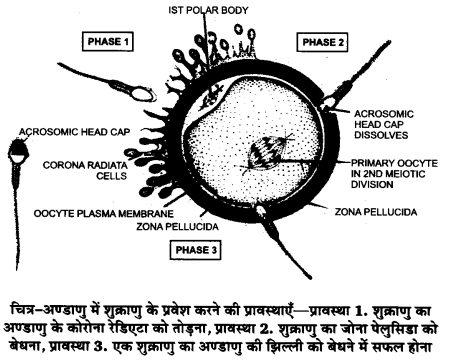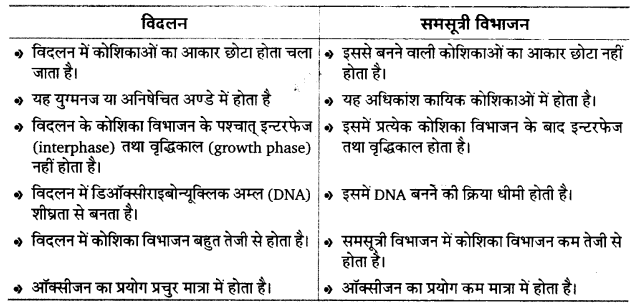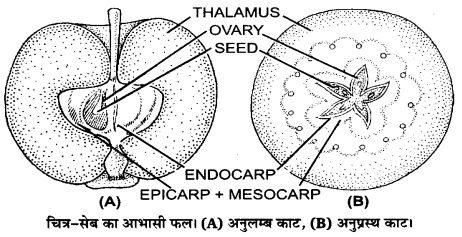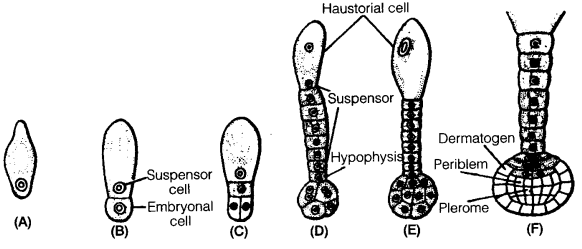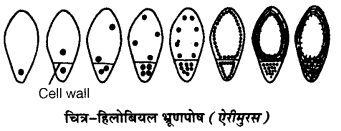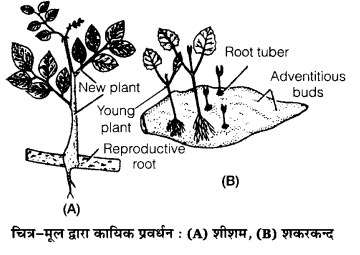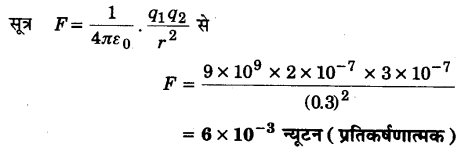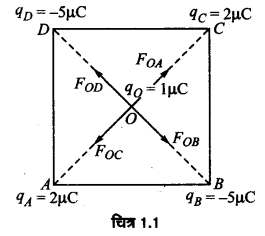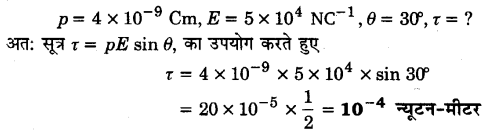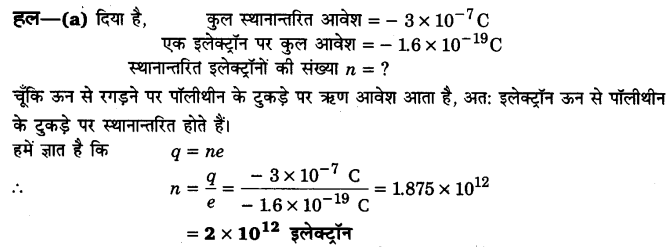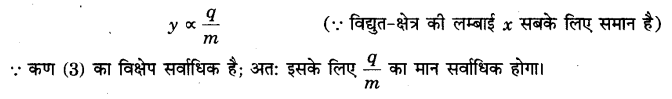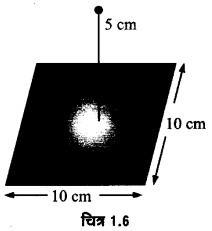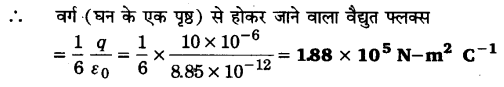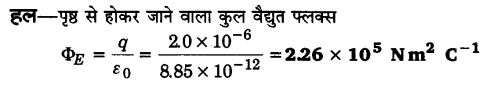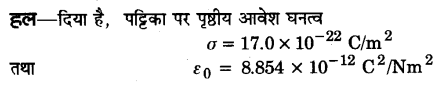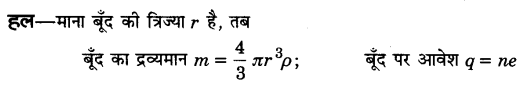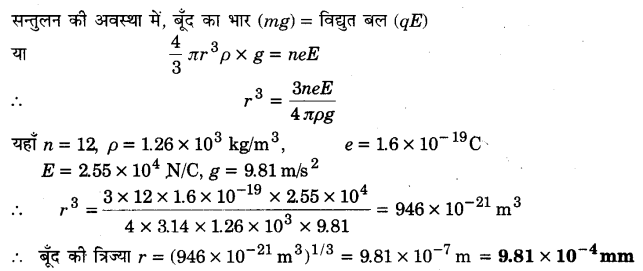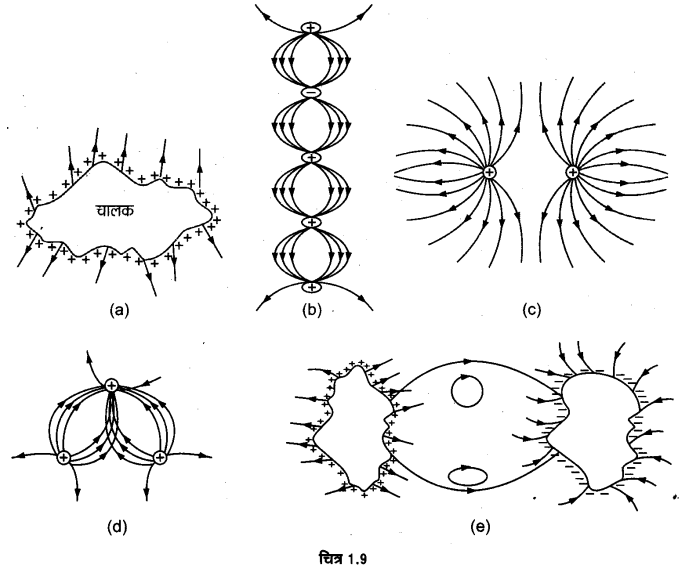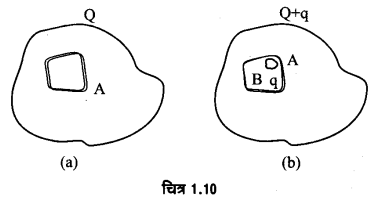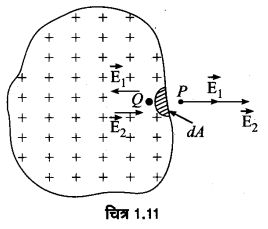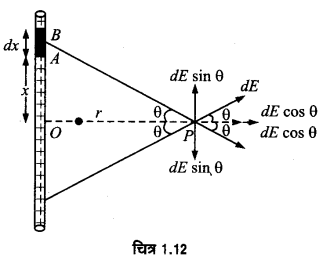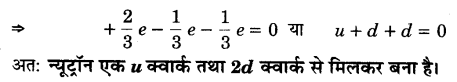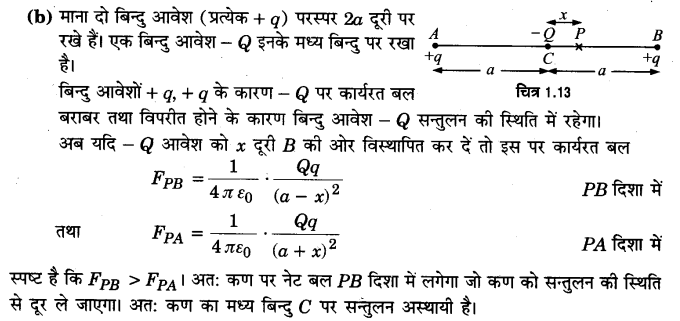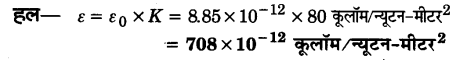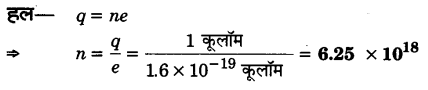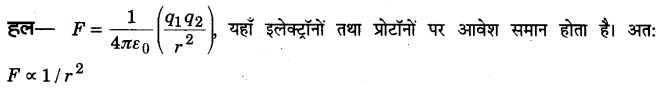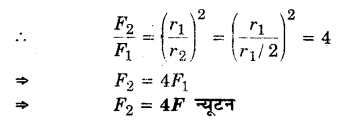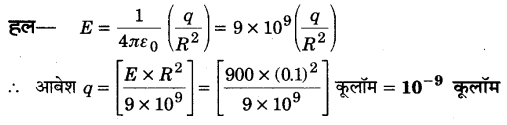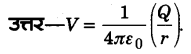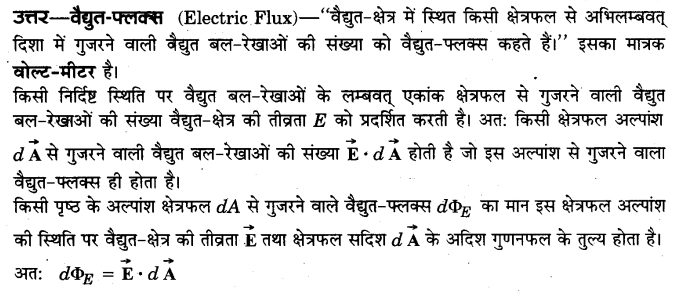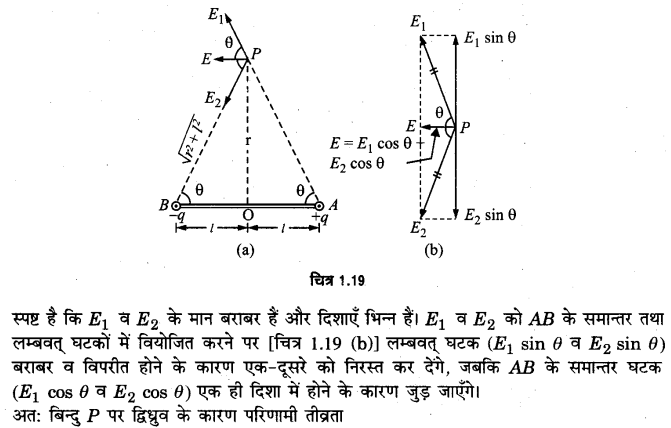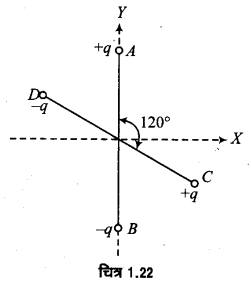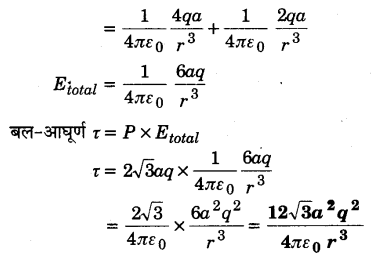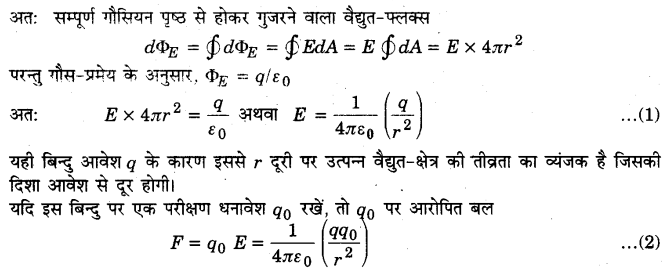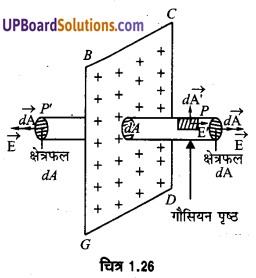UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था) are part of UP Board Solutions for Class 11 Sociology. Here we have given UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था)
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 11 |
| Subject |
Sociology |
| Chapter |
Chapter 2 |
| Chapter Name |
Social Change and Social Order in Rural and Urban Society |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था)
पाठ्य-पुस्तक के प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के लिए कारण दें।
उत्तर
भारत जैसे परंपरागत समाज में भी सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक रूप से एक नवीन घटना है। अधिकांश सामाजिक परिवर्तनों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल को माना जाता है। इसी काल में परंपरागत भारतीय समाज के सभी प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से गाँव, जाति तथा संयुक्त परिवार, में दूरगामी एवं तीव्र परिवर्तन प्रारंभ हुए। नगरीकरण, औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, जैसी प्रक्रियाएँ भारत में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी रही हैं। प्रजातंत्रीकरण एवं राजनीतिकरण ने भी समाज में हो रहे परिवर्तनों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता दी है।
सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो महत्त्वपूर्ण है अर्थात् जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दें। परिवर्तन का ‘बड़ा होना इस बात से नहीं मापा जाता है कि वह कितना परिवर्तन लाता है, अपितु यह परिवर्तन के पैमाने में मापा जाता है अर्थात् परिवर्तन समाज के कितने बड़े भाग को परिवर्तित करता है। यदि वह समाज के अधिकांश भाग को प्रभावित करता है तो उसे हम तीव्र सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
यह सही है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना भी है। समाजशास्त्र का उद्भव ही इस तीव्र सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाज में होने वाले बदलाव को समझने के प्रयास से हुआ है। तीन ऐसी प्रमुख घटनाएँ मानी जाती हैं जो तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं-“औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा ज्ञानोदय। इन घटनाओं ने न केवल पूरे यूरोप के सामजों को हिलाकर रख दिया अपितु गैर-यूरोपीय समाजों पर भी इनका दूरगामी प्रभाव पंड़ा। चूंकि इन घटनाओं का संबंध पिछली दो-तीन शताब्दियों से ही है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन को नवीन घटना माना जाता है। इससे पहले समाज में इतने व्यापक स्तपर पर कभी भी परिवर्तन नहीं हुए थे।

प्रश्न 2.
सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है?
उत्तर
‘सामाजिक परिवर्तन’ समाजशास्त्र की एक विशिष्ट संकल्पना है। इस नाते समाजशास्त्र में इसका उपयोग भी विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, “सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है। भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हों, या प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कार से हुए हों।” वस्तुत: सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाला परिवर्तन है जिससे सामाजिक संबंध और सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
‘सामाजिक परिवर्तन’ एक सामान्य संकल्पना है जिसका प्रयोग किसी भी ऐसे परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य संकल्पना द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन अन्य परिवर्तनों से भिन्न है। उदाहरणार्थ-यह आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से भिन्न है। इसी भाँति, यह भौगोलिक या संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से भिन्न है। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा है।
अन्य परिवर्तनों से भिन्न होने के बावजूद एक विस्तृत संकल्पना होने के नाते सामाजिक परिवर्तन को उनसे अलग कर पाना कठिन है। इतना ही नहीं, अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक कारण सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ-श्रम-विभाजन का विकास एक आर्थिक परिवर्तन है परंतु इसका अध्ययन समाजशास्त्र में भी इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार है परंतु समाजशास्त्र में इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह व्यवहार अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है।

प्रश्न 3.
संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
संरचनात्मक परिवर्तन से अंभिप्राय सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी इकाई के अंगों की क्रमबद्धता से है। समाज में व्यक्ति आपसी संबंधों में बँधकर उपसमूहों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उपसमूह आपस में बँधकर समूहों का निर्माण करते। हैं। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना, इसकी संस्थाओं अथवा नियमों, जिनसे संरचना अपना स्थायित्व बनाए रखती है, में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इनको हम संरचनातमक परिवर्तन नहीं कहते हैं। यदि मूल्यों एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संरचना को परविर्तित कर दें तो इन्हें भी संरचनात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों से संपूर्ण भारतीय सामाजिक संरचना परिवर्तित हुई है क्योंकि इनसे जुड़े मूल्यों एवं मान्यताओं के बदलते ही परंपरागत सामाजिक संरचना का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है।
इसी प्रकार, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं की परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन प्रक्रियाओं ने भारतीय सामाजिक संरचना के लगभग सभी परंपरागत लक्षणों को परिवर्तित किया है। उदाहरणार्थ-जातीय श्रेणियों में पाए जाने वाले संस्तरण पर आधारित परंपरागत सामाजिक संरचना जातीय निषेधों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिवर्तित हो गई हैं।
जिंसंबैर्ग (Ginsberg) के अनुसार, “सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, अर्थात् समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित है।”
प्रश्न 4.
पर्यावरण संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए।
उत्तर
‘पर्यावरण’ शब्द दो शब्दों से बना होता है – ‘परि’ + ‘आवरण’। ‘परि’ शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से’ एवं ‘आवरण’ शब्द का अर्थ होता है। ‘ढके या घेरे हुए’। अन्य शब्दों में, पर्यावरण शब्द का अर्थ वह वस्तु है, जो हमसे अलग होने पर भी हमें चारों ओर से ढके या घेरे रहती हैं। इस प्रकार, किसी जीव या वस्तु को जो-जो वस्तुएँ, विषय, जीव एवं व्यक्ति आदि प्रभावित करते हैं, वे सब उसका पर्यावरण हैं। जिसबर्ट (Gisbert) के अनुसार, “प्रत्येक वह वस्तु, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, पर्यावरण है।” प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर सदैव महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता रहा है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन लाने में पर्यावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा समुद्री लहरें (जैसे सुनामी लहरें) समाज को पूर्णरूपेण बदलकर रख देते हैं। यह बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं अर्थात् स्थायी होते हैं तथा चीजों को वापस अपनी पूर्वस्थिति में नहीं आने देते।
उदाहरणार्थ-दिसम्बर 2004 में सुनामी लहरों की चपेट में श्रीलंका, इंडोनेशिया, अंडमान द्वीप तथा तमिलनाडु के कुछ भाग आ गए जिससे हजारों लोग मारे गए और लाखों लोगों का व्यवसाय नष्ट हो गया। यह संभव है कि उनमें से कुछ लोग, पुन: उन व्यवसायों को नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गाँवों में सामाजिक संरचना पूर्णत बदल जाएगा। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं जिन्होंने समाज को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण एशिया स्थित खाड़ी के देशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज की संरचना को बदलकर रख दिया है। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल सपंदा के बिना बिल्कुल अलग होती।
प्रश्न 5.
वे कौन-से परिवर्तन हैं जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं?
उत्तर
तकनीक (प्रौद्योगिकी) तथा अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का स्रोत रहे हैं। तकनीकी प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करने, उसके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में हमारी सहायता करती है। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की भाँति प्राकृतिक कारकों (जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज) की तरह प्रभावी हो सकते हैं। औद्योगिक क्रांति एकं तकनीकी परिवर्तन ही था जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया अपितु सामाजिक संरचना को भी हिला दिया। वाष्प शक्ति की खोज ने बड़े उद्योगों को उस ताकत से परिचित कराया जो न केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी, अपितु बिना रुकावट के चलने वाली भी थी। इसी शक्ति से यातायात के साधनों का विकास हुआ जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल दिया। वेब्लन जैसे विद्वानों ने तो तकनीक को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्रोत मानी है।
कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों जो कि प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते, का भी समाज को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। नकदी फसलों (जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास या सब्जियों की खेती) ने श्रम के लिए भारी माँग उत्पन्न की। इस माँग ने 17वी-19वीं शताब्दी के मध्य दासता जैसी संस्था को विकसित किया तथा अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के बीच दासों का व्यापार प्रारंभ हो गया। भारत में भी असम के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकतर लोग पूर्वी भारत (विशेषकर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी) के थे, जिन्हें बाध्य होकर श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा।

प्रश्न 6.
सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है?
उत्तर
सामाजिक व्यवस्था को परस्पर अंत:क्रियारत व्यक्तियों अथवा समूहों का कुलक (Set) कहा जा सकता है। यह एक ऐसा कुलक है जिसे सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता है एवं जिसका व्यक्तियों (जो इस कुलक का निर्माण करते हैं) से भिन्न अपना पृथक् अस्तित्व है। स्मेलसर (Smelser) के अनुसार, “सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय संरचनात्मक तत्त्वों से प्रतिमानित संबंधों का एक ऐसा कुलक है जिनमें एक तत्त्व में परिवर्तन इन्य इकाइयों पर अनुकूलन के लिए दबाव डालने अथवा इन्हें भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में स्थायित्व बनाए। रखने का कार्य करती है। स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि समाज के विभिन्न अंग कमोबेश वैसे ही बने रहें जैसे वे हैं अर्थात् व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएँ एक ही प्रकार के परिणाम दें तथा साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएँ पूर्वानुमानित’ रूप में आचरण करें। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों एवं मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। इन मूल्यों एवं मानदंडों को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आने वाली पीढ़ी को हस्तांरित किया जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा सामाजिक व्यवस्था अपनी निरंतरता सुनिश्चित करती है।
सामाजिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक परिवर्तन का भी विरोध इसलिए किया जाता है ताकि व्यवस्था में विघटन की परिस्थिति विकसित न हो पाए। इसलिए व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियाँ परिवर्तन का प्रतिरोध कती हैं तथा उसे विनियमित करने का प्रयास करती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक संरचना एवं स्तरीकरण की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के शासक प्रभावशाली वर्ग अधिकतर उन सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं। वे स्थायित्व में अपना हित समझते हैं। दूसरी ओर, अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों को हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियाँ अधिकांशत: अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती है तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। इससे भी समाज में स्थिरता बनी रहती है।
सामाजिक व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों का स्थायित्व बनाए रखने की दृष्टि से सदैव यह प्रयास रहता है कि व्यक्ति समाज के नियमों तथा मानदंडों का स्वतः पालन करें। यदि ऐसा संभव न हो तो सामाजिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को इन्हें मानने के लिए बाध्य भी किया जा सके। इस प्रकार, सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है।
प्रश्न 7.
सत्ता क्या है तथा यह प्रभुता एवं कानून से कैसे संबंधित है?
उत्तर
सत्ता का अर्थ वैध शक्ति से है। इसलिए वैधता को समाजशास्त्र की प्रमुख संकल्पना मानी जाता है। वैधता ही शक्ति संतुलन में अंतर्निहित होती है। समाज में ऐसी चीजें जो वैध हैं, वे उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। ‘वैधता’ अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। यदि व्यक्ति के शक्ति प्रयोग करने के अधिकार के पीछे वैधता है तो इसे शक्ति न कहकर ‘सत्ता’ कहते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता को कानूनी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरणार्थ-एक पुलिस अधिकारी, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक आदि सभी व्यक्ति अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। कचहरी में जज की आज्ञा का पालन उनके पद में निहित सत्ता के कारण करना पड़ता है। कचहरी से बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की भाँति है। वेबर ने काननी सत्ता के अतिरिक्त परंपरागत एवं चमत्कारिक सत्ता का भी उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति को वैधता प्रदान करने में कानून के साथ-साथ परंपराओं एवं चमत्कारों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
सत्ता एवं कानून में गहरा संबंध पाया जाता है। सत्ता को स्थायित्व बनाने में कानून की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून से डर से ही व्यक्ति सत्ता का अनुपालन करते हैं। यदि सत्ता से कानूनी वैधता वापस ले ली जाए तो वह सत्ता नहीं रहती तथा हो सकता है प्रभुत्व का रूप ग्रहण कर ले। प्रभुत्व में कानून की भूमिका नहीं होती अपितु इसमें ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ का नियम लागू होता है। प्रभुता या प्रभुत्व के साथ कानूनी शक्ति अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। प्रभुत्व अवैध शक्ति के रूप में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ-कालोनी में किसी गुंडे का प्रभुत्व कालोनी वालों को बहुत-सी ऐसी बातें मानने के लिए विवश कर देता है जिसे वे अन्यथा स्वीकार न करें। उस गुंडे के प्रभुत्व का कारण कानूनी सत्ता न होकर उसकी अपनी गुंडागुर्दी (मसस्ल पॉवर) है। कालोनी वाले जानते हैं कि यदि उसकी बात न मानी जाए तो वह लड़ाई-झगड़ा कर सकता है अथवा तोड़-फोड़ पर उतारू हो सकता है।

प्रश्न 8.
गाँव, कस्बा तथा नगर एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
उत्तर
गाँव का अर्थ परिवारों का वह समूह कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित होता है तथा जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। गाँव की एक निश्चित सीमा होती है तथा गाँववासी इस सीमा
के प्रति सचेत होते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से पता होता है कि उनके गाँव की सीमा ही उसे दूसरे गाँवो से पृथक् करती है। इसी सीमा में उस गाँव के व्यक्ति निवास करते हैं, कृषि तथा इससे संबंधित व्यवसाय करते हैं तथा अन्य कार्यों का संपादन करते हैं। सिम्स (Sims) के अनुसार, “गाँव वह नाम है, जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है।”
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गाँवों का उद्भव सामाज़िक संरचना में आए उन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ जहाँ खानाबदोशी जीवन की पद्धति, जो शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में गाँव तथा नगर बसावट के दो प्रमुख आधार जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि-आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात हैं। गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित व्यवसायों पर आधारित होती है।
नगर से अभिप्राय एक ऐसी केंद्रीयकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। नगर की परिभाषा देना भी एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। सोमबर्ट (Sombart) ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए कहा हुए इस संदर्भ में कहा है-“नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं। निश्चित रूप से नगर का विस्तार गाँव की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र पर होता है।
किंग्स्ले डेविस (Kingsley Davis) का कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की उपज होती है। उनके अनुसार नगर ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है। यह कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है।
कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा और नगर मुख्यत: एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं जहाँ अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। कस्बों का आकार नगरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गाँवों के लोगों की प्रवृत्तियाँ नगरीकृत हो जाती हैं तो उन्हें गाँव न कहकर ‘कस्बा’ कहा जाता है। इस प्रकार, कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने जीवनक्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों प्रकार के तत्त्वों को अंतर्निहित करता है। बर्गल (Bergal) के शब्दों में, “कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधपित्य रखता है।
प्रश्न 9.
ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर
ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। इन विशेषताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-
1. प्राथमिक समूहों को महत्त्व – ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का महत्त्व अधिक होता है। पारिवारिकता ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण का एकमात्र साधन परिवार ही है। परिवार के मुखिया का नियंत्रण सभी पर होता है। परिवार की परंपराओं का ध्यान रखकर प्रत्येक कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर पारिवारिक हितों का ध्यान रखा जाता है।
2. कम जनसंख्या – ग्रामीण क्षेत्र में केवल कुछ सीमित परिवारों के ही सदस्य निवास करते हैं। और कृषि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। अन्य कोई उद्योग-धंधे न होने के कारण बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ जाकर कम ही निवास करता है। अतएव ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है।
3. कृषि व्यवसाय – ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करनी है अतः गाँव के लोग प्रकृति के पुजारी हैं और अपना गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते हैं अतएव
ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति पूजा पाई जाती है और गतिशीलता का प्रायः अभाव पाया जाता है।
4. प्रकृति से निकटता – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति प्रात:काल से संध्या तक अपने खेतों में काम करते हैं। इसलिए उनकी प्रकृति से निकटता बनी रहती है। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामवासी कृषि के लिए भी प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं।
5. समान संस्कृति – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति एक-दूसरे को जानते हैं। उन सबका रहन-सहन, खान-पान, उठने-बैठने आदि का तरीका लगभग एक-सा ही होता है। वहाँ सभी रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि को एक ही तरीके से मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समान संस्कृति के लोग रहते हैं।
6. जाति व्यवस्था की प्रधानता – ग्रामीण क्षेत्र पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में गतिशीलता भी कम पायी जाती है, अतएव जाति की सभी विशेषताएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को संगठन जाति पर निर्भर है। जाति पंचायतों का ही वहाँ पर महत्त्व है।
7. प्राचीन विश्वासों की मान्यता – ग्रामीण क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम संस्कृति के दर्शन हाते हैं। जाँद-टोना, जंतर-मंतर, भूत-प्रेत, पूजा आदि को प्रचलने आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक रोगों को भी भगवा की इच्छा समझा जाता है और इसलिए बहुत काल तक उनका इलाज नहीं किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि रोग हमारे पूर्वजन्म के दुष्कर्मों का प्रतिफल है।
8. संयुक्त परिवार की व्यवस्था – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का भी महत्त्व है। कृषि एक ऐसा कार्य है। जिसमें अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अतएव ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मीयता पायी जाती है। इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार व्यवस्था पायी जाती है। संयुक्त परिवारों में हो रहे विघटन का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व्यवसाय के कारण ही बहुत कम है।
9. विवाह की पवित्रता – ग्रामीण क्षेत्र में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और पति-पत्नी के संबंधों को पूर्वजन्म का संस्कार माना जाता है। इसलिए एकविवाही परिवारों को महत्त्व दिया जाता है। और स्त्री अपने पति को देवता मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह-विच्छेद नहीं होते अथवा बहुत ही कम होते हैं।
10. कर्मवाद तथा भाग्यवाद में विश्वास – ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों का दृढ़ विश्वास रहता है कि | जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेंगे और हमारे भाग्य में विद्याता ने जो लिख दिया है वह अवश्य ही होगा। इसलिए वे बहुत-सी बातों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। कर्मवाद एवं भौग्यवाद में विश्वास के कारण ग्रामवासी अधिक रूढ़िवादी होते हैं।
11. सरल जीवन – ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन में बनावट नहीं होती, उनका अंदर व बाहर से व्यवहार समान ही होता है। साधारणतया सरल एवं निष्कपट जीवन उनकी मुख्य विशेषता है।
गाँवों में नगरों की अपेक्षा परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना अधिक देखने को मिलती है।
12. जजमानी प्रथा – ग्रामीण क्षेत्र में भूमिपति कृषक या जमींदार खेती करते हैं और भूमिहीन लोग उन जमींदारों की कृषि कार्य में सहायता करते हैं जिसके बदले भूमिपति उनको समय-समय पर अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करता है। उनके बच्चों के विवाह आदि के उत्सवों पर भी जजमान अपने परिजनों की सहायता करता है। वह कृषक ‘जजमान’ कहलाता है और अन्य उसके सहायक लौहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि ‘परिजन’ कहलाते हैं। इस व्यवस्था को जजमानी प्रथा कहते हैं।
13. अनौपचारिक संबंध – ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक समूहों का विशेष महत्व है। परिवार प्राथमिक समूह का रूप है। परिवार के सदस्यों में रक्त के संबंध पाए जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति | को प्रत्यक्ष रूप से जानता है अतएव उनके संबंधों में अनौपचारिकता पायी जाती है।

प्रश्न 10.
नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं?
उत्तर
नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-
1. बाल अपराध – नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक असमानता, अपरिचय का वातावरण, अत्यधिक जनसंख्या, माता-पिता एवं विद्यालयों के नियंत्रण में शिथिलता आदि अनेक कारणों से बालक अपराधी प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में बाल अपराध एक प्रमुख समस्या है तथा इस पर प्रभावी नियंत्रण रखना प्रशासन के लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाता है।
2. अपराध – बाल अपराध की भाँति नगरीय क्षेत्रों में अपराध एवं श्वेतवसन अपराध भी अधिक होते हैं। आए दिन नगरों में दिन-दहाड़े चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, चेन खींचने अत्यधिक की घटना अखबारों में देखी जा सकती है। अपराधी इन कार्यों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं तथा वह इस पर प्रभावी अंकुश नहीं रख पाता।
3. मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन – मद्यपान एवं मादक द्रव्ये व्यसन भी नगरीय क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। जगह-जगह पर शराब के ठेकों का खोला जाना तथा मादक द्रव्यों का गैर-कानूनी रूप से विक्रय नगरीय क्षेत्रों में इस समस्या का प्रमुख कारण है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों में मादक द्रव्य व्यसन के विस्तार से सभी चिंतित हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण रखना भी एक चुनौती है।
4. भ्रष्टाचार – नगरीय क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। काम करने हेतु सभी दफ्तरों में सुविधा शुल्क के नाम से पैसे लिए जाते हैं। गैर-कानूनी एवं असामाजिक काम करने वाले लोग पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को घूस देते हैं अथवा उनसे इन कार्यों को करने हेतु महीना बाँध लेते हैं इसीलिए नगरीय क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा हैं यह भी एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने हेतु न तो साधन उपलब्ध है और न ही कोई प्रभावशाली अभिकरण।
5. गन्दी बस्तियाँ – नगरीय क्षेत्रों में एक तो जनसंख्या अत्यधिक होती है तथा दूसरे अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण अधिकांश उद्योग भी इन्हीं क्षेत्रों में खोले जाते हैं। इससे आवास समस्या विकसित हो जाती है जो अनाधिकृत गन्दी बस्तियों के रूप में प्रतिफलित होती हैं। इन गन्दी बस्तियों का वातावरण ठीक नहीं होता है तथा इनमें अनैतिकता का बोलबाला होता है। इसका बच्चों एवं वहाँ रहने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गन्दी बस्तियों को हटाना अथवा इनका विनियमितीकरण करना प्रत्येक बड़े नगर के लिए एक प्रमुख समस्या है।
6. वेश्यावृत्ति – नगरीय क्षेत्रों की चुनौतियों एवं समस्याओं में वेश्यावृत्ति भी प्रमुख है। अधिकांश नगरों में ‘लाल बत्ती क्षेत्र है जहाँ पर संगठित रूप से वेश्याओं के अड्डों का संचालन किया जाता है। इतना ही नहीं, होटलों एवं मकानों में गैर-कानूनी रूप से चलने वाले कालगर्ल रैकेट भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। इन पर भी अब तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण नहीं रख पाए हैं।
7. पारिवारिक विघटन – नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अनेक एकाकी परिवारों में विभाजित होते जा रहे हैं। पति-पत्नी दोनों को बाहर नौकरी करना, घर पर अधिकांश समय दोनों का न होना, दोनों में वैचारिक मतभेद होना आदि नगरीय क्षेत्रों के परिवारों के सामान्य लक्षण है। कामकाजी महिलाएँ भूमिका-संघर्ष की शिकार हो जाती है तथा पारिवारिक विघटन का सबसे अधिक बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्रों में बुजुर्गों की समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। परिवार वाले उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते तथा सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि उनके लिए अलग वृद्धाश्रम खोले जाएँ यह भी नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख चुनौती बन गया है।
8. पर्यावरणीय प्रदूषण – नगरीय क्षेत्रों में वाहन अधिक होते हैं जिनसे निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। विकास के नाम पर बहुमंजिली इमारतों एवं उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि पर्यावरणीय संतुलन हेतु पेड़ लगाने पर कम। उद्योगों से निकलने वाला धुआँ भी प्रदूषण का कारण है। नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना भी एक चुनौती है जिसका सामना अधिकांश बड़े नगर नहीं कर पा रहे हैं।
क्रियाकलाप आधारित प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
अपने बड़ों से बात कीजिए तथा अपने जीवन से संबंधित उन चीजों की सूची बनाइए जो उस समय नहीं थीं, जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे अथवा तब अस्तित्व में नहीं थीं जब आपके नाना-नानी/दादा-दादी आपकी उम्र के थे? (क्रियाकलाप 1)
उत्तर
जब नाना-नानी/दादा-दादी आपकी उम्र के थे तब आधुनिक समय में उपलब्ध अनेक चीजें नहीं थी। उदाहरणार्थ-न तो बिजली थी और न ही बिजली से चलने वाले उपकरण। सारा काम हाथ से करना पड़ता था और उत्पादन हेतु मानवीय शक्ति के साथ-साथ पशु शक्ति को भी अधिकांशतः प्रयोग किया जाता था। आने-जाने के साधन नहीं थे तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए पैदल, घोड़ों पर अथवा ताँगों पर जाने का प्रचलन अधिक था। न अच्छी सड़कें थी, न घर पर पानी की उचित व्यवस्था थी और न ही स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध थीं। रेलगाड़ी, टी०वी०, फ्रिज इत्यादि तक का अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं था।
जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के थे तब उस नाना-नानी/दादा-दादी के समय से तो अधिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं, परंतु आज की तुलना में वे भी अपर्याप्त थीं। उदाहरणार्थ-नगरीय क्षेत्रों में बिजली थी तथा बिजली से चलने वाले उपकरण भी थे। श्याम-श्वेत टेलीविजन प्रचलित था तथा देखने हेतु चैनल एवं कार्यक्रम अत्यंत सीमित थे। न रंगीन टी०वी० का प्रचलन था, न दूध प्लास्टिक की थैलियों में मिलता था और न ही कपड़ों में जिप का प्रयोग होता था। प्लस्टिक की बाल्टी एवं मग इत्यादि का प्रचलन नहीं था। खाना बनाने के लिए गैस नहीं थी तथा लकड़ी एवं कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। स्टील, ऐलुमिनियम आदि के बर्तनों के स्थान पर पीतल एवं मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक होता था। आप अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी से बात करके वस्तुओं की इस सूची को और आगे बढ़ा सकते हैं।
प्रश्न 2.
फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आई? क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा दूरगामी थे कि ‘क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य हो सकें? (क्रियाकलाप 2)
उत्तर
पूरे विश्व की कायापलट करने वाली प्रक्रियाओं में फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति का प्रमुख स्थान है। इन दोनों के द्वारा होने वाले परिवर्तनों का संबंध समाज के किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। सभी क्षेत्रों पर इनके दूरगामी प्रभावों के कारण ही इनसे होने वाले परिवर्तनों को ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ कहा जाता है।
अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। उस समय सामन्तों तथा उच्च पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे लोग वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यततीत करते थे, लेकिन जनसाधारण वर्ग की दशा बड़ी शोचनीय थी और उसका जीवन कष्टों से भरपूर था। इसके परिणामस्वरूप 1789 ई० में फ्रांस में एक खूनी क्रांति हुई, जिसने शीघ्र ही भीषण रूप धारण कर लिया। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। इस क्रांति में फ्रांस का सम्राट लुई सोलहवाँ, उसकी रानी मेरी अंतायनेत और उनके हजारों साथियों को गुलोटिन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्रांति के कारण 25 वर्ष तक संपूर्ण यूरोप युद्ध की आग में जलता रहा। हजारों नगर बरबाद हो गए और लाखों व्यक्ति मारे गए। यह संपूर्ण रक्तपात, जो बास्तील के पतन (14 जुलाई, 1789 ई०) से आंरभ हुआ और वाटरलू के युद्ध (18 जून, 1815 ई०) के बाद समाप्त हुआ, फ्रांस की क्रांति का घटनाक्रम कहलाता है।
फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। इनमें सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था (Ancient Regime) का अंत, मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत, मानव जाति की स्वाधीनता के लिए ‘मानव और नागरिकों के जन्मजात अधिकारों की घोषणा’ (27 अगस्त, 1789 ई०), सारे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का विकास, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया जाना, इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेशी नीति का प्रभावित होना, समाजवादी व्यवस्था का मार्ग खोलना तथा कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में होने वाली अभूतपूर्व उपलब्धियाँ प्रमुख हैं।
फ्रांस की क्रांति की भाँति, इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में आश्चर्यजनक परिवर्तन से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति ने भी बड़े पैमाने के उद्योगों का सूत्रपात किया। इसके परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को क्रान्तिकारी परिवर्तन’ कहा जाता है। इस क्रांति से नए समाज का जन्म हुआ। समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, रहन-सहन का स्तर, खान-पान, धार्मिक विश्वास, विज्ञान तथा साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिससे एक नए समाज का प्रादुर्भाव हुआ। न केवल मनुष्य को अपना जीवन बिताने में अधिक सुख तथा सुविधा प्राप्त हुई, अपितु संयुक्त परिवार समाप्त होने प्रारंभ हो गए तथा उनका स्थान पर छोटे-छोटे परिवारों ने ले लिया। महिलाओं को भी स्वतंत्र प्राप्त हुई। उन्हें समान अधिकार मिलने प्रारंभ हुए तथा वे स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने लगीं। मध्यम वर्ग का उदय भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों का जीवन बड़ा संकटमय बना दिया। उनको न केवल वेतन कम दिया जाता था अपितु उनके जीवन की सुरक्षा की चिंता पूँजीपतियों को नहीं थीं।
लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि, वर्ग-संघर्ष को उदय, औद्योगिक नगरों का विकास, घरेलू उद्योग-धंधों का विनाश भी औद्योगिक क्रांति के दूरगामी प्रभाव रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने जहाँ एक ओर लोगों के लिए रोजगार के मार्ग खोले वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। मशीनों के लग जाने के कारण कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिको की संख्या घटने लगी। आर्थिक दृष्टि से संसार के सभी राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता की ऐसी लहर दौड़ी कि वे औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से दौड़ लगाने लगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा; अत: यूरोप के देशों ने उत्पादित माल के खपाने तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। इससे साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा मिला। इन सब परिवर्तनों के कारण ही औद्योगिक क्रांति के परिणामों को ‘क्रांतिकारी परिवर्तनों की संज्ञा दी गई है।

प्रश्न 3.
अन्य किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, जो | क्रांतिकारी परिवर्तन के योग्य नहीं है? वे क्यों योग्य नहीं है? (क्रियाकलाप 2)
उत्तर
ऐसे परिवर्तन, जो अधिक विस्तृत नहीं होते तथा जिनका प्रभाव समाज के बड़े हिस्से पर नहीं पड़ता, ‘क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहलाते। उदाहरणार्थ-उविकासीय परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कहा जाता। उविकास ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जो काफी लंबे समय तक धीरे-धीरे होता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त यह शब्द जीवित प्राणियों के विकसित होने की प्रक्रिया को इंगित करता है। कई शताब्दियों अथवा कभी-कभी सहस्राब्दियों में धीरे-धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलने की प्रक्रिया उविकास कहलाती है। इसमें डार्विन ने ‘योग्यतम की उत्तरजीविता’ के विचार पर बल दिया; अर्थात् केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढाल लेते हैं अथवा ऐसी धीमी गति से करते हैं और लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। उदूविकासीय परिवर्तन न तो शीघ्र अथवा अचानक होते हैं और न ही इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है; अतः ये परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति अथवा रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की भाँति ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ कहलाने योग्य नहीं हैं।
प्रश्न 4.
क्या आपने ऐसे तकनीकी परिवर्तनों पर ध्यान दिया है जिनका आपके सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हो? (क्रियाकलाप 3)
उत्तर
तकनीकी परिवर्तन को हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तकनीकी परिवर्तनों ने हमारे जीवन को आरामदायक बना दिया है। आज गर्मी से बचने के लिए एक तरफ पंखे, कूलर एवं एयर कंडीशनर है तो दूसरी ओर सर्दी से बचने के लिए हीटर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए यातायात के विभिन्न साधन (बस, कार, रेल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज इत्यादि) उपलब्ध है। पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी घर बैठे अखबारों अथवा टेलीविजन के माध्यम से मिल जाती है। टेलीविजन के कार्यक्रम को रिमोट कंट्रोल द्वारा बदला जा सकता है तथा इसके चलाने एवं बंद होने को भी रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं धारावाहिकों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
पहनने के लिए कपड़ों की क्वालिटी में अत्यधिक परिवर्तन आया है तथा हम नित नए फैशनों को अपना रहे हैं। खान-पान पर तकनीकी परिवर्तनों का गहरा प्रभाव पड़ा है। जमीन पर बैठने के स्थान पर आज परिवार के सदस्य एक साथ खाने की मेज पर बैठकर खाना खाते देखे जा सकते हैं। घर पर कंप्यूटर पर बैठे-बैठे इंटरनेट के माध्यम से ई-मेल द्वारा पत्र-व्यवहार किया जा सकता है, रेलवे या हवाई जहाज के टिकट बुक कराए जा सकते हैं। बैंकों से कारोबार किया जा सकता है अथवा वस्तुओं की खरीद-फरोख्त की जा सकती है। इस प्रकार, तकनीकी परिवर्तनों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है तथा इनसे हमारी संपूर्ण जीवन-शैली ही परिवर्तित हो गई है।
प्रश्न 5.
आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए जहाँ आप चीजों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे? क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहाँ आप चीजों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? कारण सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं? (क्रियाकलाप 4)
उत्तर
जीवन के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिनमें प्रयोग होने वाली चीजों को हम जल्दी बदलना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ-हम अपने परिवार को नहीं बदलना चाहते। हम नहीं चाहते कि स्कूल से घर आने के बाद हमें यह पता चले कि हमारे माता-पिता से भिन्न कोई और हमारे माता-पिता के रूप में या भाई-बहन के रूप में हमारे घर पर बैठा है। इसी भाँति, हम नहीं चाहते कि जो खेल हमें पसंद है उसके नियम रोज बदल जाएँ। हम नित्य प्रति खाने की चीजों को नहीं बदलते। हमारा प्रयास यह रहता है कि जो खाने की वस्तुएँ हमें पसंद हैं वे जल्दी-जल्दी हमें मिलती रहें। इसी भाँति, यदि हर रोज जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन हो जाए अथवा जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वह बदल जाएँ तो सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी।
सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व रखने के कारण ही हम नहीं चाहते कि हमारी मान्यताएँ, आदर्श एवं रीति-रिवाजों में प्रतिदिन परिवर्तन हो जाए। ऐसा होने पर सामाजिक विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित नहीं हो पाएगी और समाज का स्थायित्व समाप्त होने लगेगा। समाज में स्थायित्व के लिए कुछ चीजों में निरंतरता होनी आवश्यक है और इसीलिए उनमें होने वाले परिवर्तनों का विरोध भी किया जाता है।
प्रश्न 6.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है? इसे कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर यह सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? (क्रियाकलाप 5)
उत्तर
2005 ई० का ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ निर्धन ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय प्रयास माना जाता है। ग्रामीण निर्धनों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, उनके लिए रोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता. उन्मूलन भारत सरकार की विकास नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ 25 दिसम्बर, 2001 ई० को प्रारंभ की गई थी। दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने, कमजोर वर्गों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रांरभ की गई यह योजना इसलिए प्रमुख विकास योजना मानी जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम-से-कम 25 प्रतिशत निर्धारित मजदूरी नकद दी जाती है।
यह कार्यक्रम निर्धन ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देकर न केवल ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने में सहायक हो रहा है अपितु इससे निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन केरने वाले परिवारों को ऊपर उठाने में भी सहायता मिल रही है। इसीलिए इस कार्यक्रम में निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के निर्धन लोगों का चयन कर उन्हें रोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराता है। यदि यह कार्यक्रम सफल हो जाता है तो ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी काफी सीमा तक कम हो सकती है। इससे निर्धन ग्रामीणों को शोषण भी रूक जाएगा तथा उन्हें ससम्माने अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर उपलब्ध हो पाएगा।
प्रश्न 7.
क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में ‘गेटेड समुदाय को देखा/सुना है, अथवा कभी उनके घर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चारदीवारी तथा गेट कब बने? क्या इसका विरोध किया गया, यदि हाँ तो किसके द्वारा? ऐसे स्थानों पर रहने के लिए लोगों के पास कौन-से कारण हैं? आपकी समझ से शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? (क्रियाकलाप 6)
उत्तर
‘गेटेड समुदाय’ एक नवीन संकल्पना है। इसका अर्थ एक ऐसे समृद्ध प्रतिवेशी समुदाय का निर्माण है जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है अर्थात् जहाँ प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदायों की अपनी समानांतर नागरिक सुविधाएँ (जैसे पानी और बिजली की सप्लाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि) होती हैं। इस प्रकार के ‘गेटेड समुदाय’ सभी नगरों एवं महानगरों में देखे जा सकते हैं। ऐसे ‘गेटेड समुदाय’ अनके कारणों से विकसित हुए हैं जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान प्रमुख है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्रजाति, नृजातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होते हैं। पहले मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्तियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति या सम्मान की पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने को इंगित करता है। मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस का समान लक्षणों वाले पड़ोस में बदल जाना ‘घैटोकरण’ कहलाता है।
भारत में अनेक नगरों में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव से मिश्रित प्रतिवेशी समुदाय एकल समुदायों में बदल गए हैं अर्थात् जिन क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ निवास करते थे अब वे अपने ही धर्म के लोगों के बीच रहना अधिक पसंद करते हैं तथा धर्म के आधार पर आवासीय क्षेत्र एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2002 ई० के दंगों के दौरान गुजरात में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द, लौकिक विचारधारा, राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्र-निर्माण के प्रबल समर्थक होते हैं वे इस प्रकार के गेटेड समुदायों का विरोध करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्र के प्रति वफादारी कम करती है तथा मानव दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाए रखने में सहायक होती है। यदि शहरी समाज में यह प्रवृत्ति बढ़ती है तो विभिन्न धर्मों, जातियों, राज्यों के लोगों में होने वाली अंत:क्रिया बाधित होगी और अंततः राष्ट्रीयता को ही आघात पहुँचेगा।

प्रश्न 8.
क्या आपने अपने पड़ोस में ‘भद्रीकरण’ देखा है। क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं। पहले उपबस्ती कैसी थी जब यह घटित हुआ? पता कीजिए। किस रूप में परिवर्तन आया है। विभिन्न सामाजिक समूहों को इसने कैसे प्रभावित किया है? किसे फायदा अथवा किसे नुकसान हुआ है? इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय कौन लेता है? (क्रियाकलाप 7)
उत्तर
‘भद्रीकरण’ (जैट्रीफिकेशन) शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से निम्नवर्गीय पड़ोस मध्यम अथवा उच्चवर्गीय पड़ोस में बदल जाता है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर के केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत-से परिवर्तन हुए हैं। नगर के 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रांरभ तक ‘शक्ति केंद्र बने रहने के पश्चात् 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक नगरीय केंद्र का पतन प्रांरभ हो गया। यहीं समय उपनगरों के विकास का भी था क्योंकि विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन कर उपनगरीय क्षेत्रों में सस्ती जमीन लेकर उसे पर आलीशान मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व के निम्नवर्ग का उपनगरीय क्षेत्र मध्यम अथवा उच्च वर्ग के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।
इस प्रवृत्ति के प्रारंभ होते ही उपनगरीय क्षेत्र (उपबस्ती क्षेत्र) की कायापलट होने लगी। कीमतें आसमान छूने लगीं तथा क्षेत्र का विकास अत्यधिक तीव्र गति से होने लगा। जीवन की सभी सुविधाएँ इन क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक उपलब्ध कराने की होड़ लग गई। इससे उन संपन्न लोगों को भी लाभ हुआ जिन्होंने नगर के अंदरूनी भाग से पलायन किया तथा उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले उस गरीब को भी जिसने अधिक कीमत पर अपनी जमीन का हिस्सा उस संपन्न व्यक्ति को बेच दिया। उसे भी अपनी शेष बची जमीन पर अच्छा मकान बनाने तथा अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का अवसर मिला। इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय अधिकांशतः संपन्न लोग ही लेते हैं। वे नगर के अंदरूनी हिस्से में सीमित आवास होने के कारण न तो अपनी उच्च जीवन-शैली को प्रदर्शित कर सकते हैं और न ही उस शानो-शौकत से रह सकते हैं जिससे कि वे रहना चाहते हैं।
परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय है?
(क) विश्व समुदाय
(ख) क्लब
(ग) गाँव
(घ) कर्मचारी संघ
उत्तर
(ग) गाँव
प्रश्न 2.
निम्नलिखित में कौन-सा समुदाय का उदाहरण नहीं है ?
(क) एक गाँव
(ख) एक परिवेश
(ग) एक नगर
(घ) एक संप्रदाय
उत्तर
(घ) एक संप्रदाय

प्रश्न 3.
नगरीयवाद का अर्थ होता है१
(क) नगरीय जनसंख्या की वृद्धि
(ख) नगरीय जीवन पद्धति
(ग) नगरों को भौतिक विकास
(घ) ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन
उत्तर
(ख) नगरीय जीवन पद्धति
प्रश्न 4.
भारतीय गाँवों में किस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं ?
(क) एकाकी परिवार
(ख) संयुक्त परिवार
(ग) आधुनिक परिवार
(घ) मिश्रित परिवार
उत्तर
(ख) संयुक्त परिवार
प्रश्न 5.
ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है
(क) कृषि पर निर्भरता
(ख) जनाधिक्य
(ग) प्रकृति से घनिष्ठ संबंध
(घ) प्राथमिक संबंधों की बहुलता
उत्तर
(ख) जनाधिक्य
प्रश्न 6.
“सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण होता है।” यह कथन किसका है?
(क) वेबलन का
(ख) ऑगबर्न को
(ग) टॉयनबी का
(घ) सोरोकिन का
उत्तर
(क) वेबलने का

प्रश्न 7.
कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है
(क) यांत्रिक प्रयोग
(ख) आर्थिक कारण
(ग) धार्मिक कारण
(घ) राजनीतिक कारण
उत्तर
(ख) आर्थिक कारण
प्रश्न 8.
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है ?
(क) जॉर्ज सी० होमंस ने
(ख) बीसेज एवं बीसेज ने
(ग) आगस्त कॉम्टे ने
(घ) रॉबर्ट बीरस्टीड ने
उत्तर
(ग) आगस्त कॉम्टे ने
प्रश्न 9.
भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर किस विद्वान ने सबसे अधिक अध्ययन किया ?
(क) डॉ० नगेन्द्र ने
(ख) सच्चिदानंद ने
(ग) एम० एन० श्रीनिवास ने
(घ) डॉ० राधाकृष्णन ने
उत्तर
(ग) एम० एन० श्रीनिवास ने
प्रश्न 10.
ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार पर की है ?
(क) सामाजिक असंतुलन
(ख) नैतिक पतन
(ग) सांस्कृतिक विलम्बना
(घ) प्रौद्योगिकीय कारक
उत्तर
(ग) सांस्कृतिक विलम्बना
प्रश्न 11.
संस्कृति की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण कौन मानता है ?
(क) सोरोकिन
(ख) मैक्स वेबर
(ग) सिमेल
(घ) मॉण्टेस्क्यू
उत्तर
(क) सोरोकिन

प्रश्न 12.
सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक कौन है ?
(क) कार्ल मार्क्स
(ख) वेबलन
(ग) जॉर्ज लुंडबर्ग
(घ) मैक्स वेबर
उत्तर
(घ) मैक्स वेबर
प्रश्न 13.
कौन-सी पुस्तक एफ० एच० गिडिंग्स द्वारा लिखी गयी है ?
(क) सोसायटी
(ख) पॉजिटिव पॉलिटी
(ग) इंडक्टिव सोशियोलॉजी
(घ) सोशियल कंट्रोल
उत्तर
(ग) इंडक्टिव सोशियोलॉजी
प्रश्न 14.
‘कल्चरल डिस ऑर्गेनाइजेशन’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) के० डेविस
(ख) इलियट एंड मैरिल
(ग) कूले
(घ) स्पेन्सर
उत्तर
(ख) इलियट एंड मैरिल
प्रश्न 15.
श्वेतवसन अपराध अवधारणा से कौन समाजशास्त्री जुड़ा है ?
(क) सदरलैण्ड
(ख) लॉम्ब्रोसो
(ग) कार्ल मार्क्स
(घ) एंजिल्स
उत्तर
(क) सदरलैण्ड
प्रश्न 16.
अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं –
या
अपराध के शास्त्रीय सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन हैं?
(क) बेन्थम
(ख) मॉण्टेस्क्यू
(ग) बकल
(घ) कार्ल मार्क्स
उत्तर
(क) बेन्थम
प्रश्न 17.
अच्छे आचरण के कारण बंदीगृह से अस्थायी मुक्ति को कहते हैं –
(क) प्रोबेशन
(ख) पैरोल
(ग) मुक्ति सहायता
(घ) आचरण मुक्ति
उत्तर
(ख) पैरोल
प्रश्न 18.
सदरलैण्ड किस पुस्तक के लेखक थे ?
(क) सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन
(ख) सोशल चेंज
(ग) प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी
(घ) सोसायटी
उत्तर
(ग) प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी
निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
उदविकास क्या है?
उत्तर
काफी लंबे समय तक धीरे-धीरे वोली उस प्रक्रिया को, जिसने जीव सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, उविकास कहा जाता है।
प्रश्न 2.
संरचना परिवर्तन किसे कहते हैं?
उत्तर
समाज की संरचना में होने वाले ऐसे परिवर्तनों को, जो उस पर दूरगामी प्रभाव डालता है, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं।

प्रश्न 3.
सत्ता का आधार क्या होता है?
उत्तर
सत्ता का आधार वैधता है। वेबर के अनुसार कानून, परंपरा तथा चमत्कार वैधता के प्रमुख आधार होते हैं।
प्रश्न 4.
कानून विरोधी उस व्यवहार को क्या कहा जाता है जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है?
उत्तर
कानून विरोधी उस व्यवहार को, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, अपराध कहा जाता है।
प्रश्न 5.
शक्ति, प्रभाव एवं सत्ता में किसे व्यापक माना जाता है?
उत्तर
प्रभाव को शक्ति एवं सत्ता की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है।
प्रश्न 6.
हिंसा का प्रमुख कारण क्या है?
उत्तर
हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा यह समाज में गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है।
प्रश्न 7.
‘दि प्रोटेस्टेंट इथिक एण्ड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
उत्तर
‘दि प्रोटेस्टेंट इथिक एण्ड दि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ नामक पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर है।
प्रश्न 8.
संरक्षित समुदाय से आप क्या समझते हैं?
उत्तर
नगरीय क्षेत्रों में उच्च एवं संपन्न वर्गों द्वारा अपने मुहल्लों के चारों ओर एक घेराबंदी कर लेने तथा आने-जाने पर नियंत्रण रखने को संरक्षित समुदाय कहते हैं।

प्रश्न 9.
भद्रीकरण किसे कहते हैं?
उत्तर
निम्नवर्ग परिवेश के मध्यम या उच्चवर्गीय परिवेश में बदल जाने को भद्रीकरण कहते हैं।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो?
उत्तर
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन, समाज की विभिन्न इकाइयों, सामाजिक संबंधों संस्थाओं इत्यादि में होने वाला परिवर्तन है। संगठन का निर्माण संरचना तथा कार्य दोनों से मिलकर होता है। सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक अंत:क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सामाजिक परिवर्तन ही कहा जाता है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है। भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हुए हों, या सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना तथा सिद्धांतों के परिवर्तन से हुए हों, या प्रसार से अथवा समूह के अंदर ही
आविष्कार से हुए हों।”
प्रश्न 2.
सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख स्रोत बताइए।
उत्तर
सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं –
1. मानसिक विकास – जनता के मानसिक विकास का साधन शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं का प्रसार जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में होगा, उस स्थान के व्यक्ति प्रबद्ध एवं विचारशील होंगे और वे समाज में प्रचलित संकीर्णताओं व रूढ़ियों की अपेक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे अपितु उनके स्थान पर नवीन विचारों को लाने का भरसक प्रयास करेंगें इस प्रकार, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जनता का जो मानसिक विकास होता है, उसी के परिणामस्वरूप प्राचीन रीति-रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है।
2. ज्ञान प्रसार के साधन – वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जिस समाज में समाचार-पत्रों, रेडियो, यातायात के साधनों तथा संचार-वाहन के साधनों की प्रचुरता होगी, वह समाज सामाजिक परिवर्तन का उतना ही शीघ्र स्वागत करेगा। वस्तुतः ये साधन ज्ञान-विज्ञान के विकास के साधन है। इन साधनों की प्रचुरता के कारण देश में नवीन विचारधाराओं को प्रसार सरलता से हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। भारत में प्राचीन मूल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन इन्हीं साधनों की देन है।
प्रश्न 3.
विलबर्ट ई० मूर द्वारा बताई गई सामाजिक परिवर्तन की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
विलबर्ट ई० मूर ने सामाजिक परिवर्तन की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनमें से चार निम्नलिखित हैं –
- सामाजिक परिवर्तन हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर धीमी गति से प्रभाव डालता है।
- सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
- सामाजिक परिवर्तन हमारे भौतिक जीवन को तीव्र गति से प्रभावित करता है। इसलिए आज भोजन व वस्त्रों में पहले से अधिक अंतर आ गया है। हम आज आकर्षक तथा भोग-विलास की वस्तुओं से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं।
- जो परिवर्तन हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है उसकी गति अधिक तीव्र होती है।

प्रश्न 4.
सामाजिक परिवर्तन को पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है?
उत्तर
पर्यावरण अनेक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। प्राकृतिक विपदाओं, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अवक्रमण का सामाजिक संरचना, व्यक्तियों के रहन-सहन, उनके व्यवसायों, उनके स्वास्थ्य इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुनामी लहरों के कारण तटीय प्रदेशों में रहने वाले अनेक लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो गए। अनुकूल पर्यावरण सामाजिक विकास में सहायक होता है, जबकि प्रतिकूल पर्यावरण सामाजिक विकास को अवरुद्ध करती है।
प्रश्न 5.
सामाजिक परिवर्तन को संस्कृति किस प्रकार से प्रोत्साहन देती है?
उत्तर
संस्कृति का संबंध उन विचारों, मूल्यों एवं मान्यताओं से होता है जो मनुष्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में सहायता प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं का समाज को व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट इथिक को यूरोप में पूँजीवाद के विकास से जोड़ा है तथा यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार धार्मिक मान्यताएँ दूरगामी आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म के प्रभाव तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव भी भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा गया है।
प्रश्न 6.
क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं?
उत्तर
ऐसे परिवर्तन, जो शीघ्र अथवा अचानक होते हैं तथा समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति तथा ज्ञानोदय से जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण इन परिवर्तनों द्वारा यूरोपीय एवं गैर-यूरोपीय समाजों की संरचना में होने वाले आमूल चूल परिवर्तन हैं। राजनीतिक क्रांतियों तथा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जिन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। सामान्य रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन’ शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए किया जाता है।
प्रश्न 7.
अपराध के दो प्रमुख तत्व बताइए।
उत्तर
अपराध के दो प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –
1. अपराध व्यावहारिक रूप में कोई ऐसा कार्य करना है जिसे समाज तथा कानून दंडनीय मानते हैं।
अन्य शब्दों में, कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक उससे बाह्य परिणाम या नुकसान न हो। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा करता है या शब्दों में कह भी देता है तो यह सोचना या कहना-मात्र अपराध नहीं होगा। कई बार कोई आदमी किसी से क्रोध में यह कह देता है कि तुझे जान से मार देंगा; तो इसका यह आशय नहीं कि उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। वास्तव में अपराध एक स्पष्ट कृत्य है।
2. अपराध के कर्ता का इरादा अपराधमय (जिसे दोषी इरादा भी कहा जाता है) होना चाहिए। • उदाहरणार्थ-वह डॉक्टर, जो रोगी के प्राण बचाने के लिए ऑपरेशन करता है परंतु इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, अपराधी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसका दोषी इरादा नहीं था।
प्रश्न 8.
सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना सुनिश्चित कीजिए।
उत्तर
सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय समाज के विभिन्न अंगों में एकीकरण से है। मानव शरीर की भाँति समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं ठीक उसी प्रकारे समाज के विभिन्न अंग अपना निर्धारित कार्य करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसमें स्थायित्व पाया जाता है। समाज के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक अंग में होने वाला परिवर्तन अन्य अंगों को प्रभावित करता है। पेरेटो (Pareto) ने इस संदर्भ में कहा है-“समाज विभिन्न शक्तियों के साम्य की एक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था समाज की वह अवस्था है जो किसी दिए हुए समय तथा परिवर्तन की उत्तरोत्तर दशाओं से प्राप्त होती है।”

प्रश्न 9.
नगरीय सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
नगरीय सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –
1. सामाजिक विजातीयता – नगरीय समुदायों की जनसंख्या विविध प्रकार के व्यवसायों में लगी होती है तथा उनके रहन-सहन एवं खान-पान, सांस्कृतिक मूल्यों तथा रीति-रिवाजों में काफी भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में अंत:क्रियाओं में हिस्सा लेता है, उससे भिनता की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाती है।
2. द्वितीयक समितियाँ – नगरीय समुदायों की दूसरी विशेषता द्वितीयक समितियाँ या साहचर्य है। द्वितीयक समितियों की प्रधानता के कारण नगरीय समुदाय के लोग परस्पर व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते। अप्रत्यक्ष व अवैयक्तिक संबंधों के कारण नगरवासियों के जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हो जाती है। मित्रों तथा परिचित व्यक्तियों से भी हमारे संबंध स्वयं में पूर्ण नहीं होते हैं।
प्रश्न 10.
संघर्ष किसे कहते हैं? समझाइए।
उत्तर
संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते है, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक परिवर्तन की उपयुक्त परिभाषा देते हुए इसकी दो मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
मैरिल एवं ऐल्ड्रिज के अनुसार, “अपने सर्वाधिक सही अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि अधिक संख्या में व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में व्यस्त हों जो कि उनके पूर्वजों के अथवा उनके अपने कार्यों से भिन्न हो, जिन्हें वे कुछ समय पूर्व तक करते थे। समाज का निर्माण प्रतिमानित मानवीय संबंधों के एक विस्तृत एवं जटिल जाल से होता है जिसमें सब लोग भाग लेते हैं। जब मानव व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया में होता है तो यह, यह कहने का ही दूसरा तरीका है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।”
सामाजिक परिवर्तन की दो मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं –
1. सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यम्भावी है – सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। तथा समयानुकूल होता रहता है। मानव स्वभाव प्रत्येक क्षण नवीनता चाहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा अवश्यंभावी है। यह किसी की इच्छा अथवा अनिच्छा पर निर्भर नहीं होता, यद्यपि आधुनिक युग में इसे नियोजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है।
2. सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है – सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष से न होकर पूर्ण समाज के जीवन से होता है। यह व्यक्तिवादी नहीं वरन् समष्टिवादी होता है। इसीलिए परिवर्तन का प्रभाव सामान्यत: संपूर्ण समाज पर पड़ता है।
प्रश्न 2.
“अपराध एक सामाजिक-कानूनी अवधारणा है।” स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
अपराधको सामाजिक तथा कानूनी रूप से ऐसा कार्य करना बताया गया है जिसे समाज तथा कानून दोनों अनुचित मानते हैं। इसी श्रेणी की परिभाषाओं को कुछ विद्वान अधिक उचित मानते हैं, क्योंकि अपराध को न तो सिर्फ कानून की दृष्टि से ही समझा जा सकता है और न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से। अपराध के सही अर्थ को जानने के लिए कानूनी तथा सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों को महत्त्व देना अति आवश्यक है। इसीलिए संभवतः आज अपराध की व्यवहार संबंधी व्याख्या अधिक मानय होने लगी है जिसमें अपराध को भी एक असामान्य वैयक्तिक व्यवहार अथवा प्रतिमान में विचलन के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, जब हम अपराध को अपराधी नियमों का उल्लंघन मानते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून अधिकतर सामाजिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। हत्या, बलात्कार, हमला व चोरी सब कानून के विरुद्ध हैं।
कानून कई बार ऐसे व्यवहार को भी अनदेखा कर देता है जिसे अधिकांश लोग गैर-सामाजिक मानते हैं; जैसे किसी लुटते या पिटाई होते व्यक्ति की सहायता न करना। अत: कोई समाज किस प्रकार के व्यवहार को कानूनी या सामाजिक रूप से निषिद्ध करेगा, यह सामाजिक आदर्शों पर आधारित होता है। लैंडिस तथा लैंडिस के अनुसार, “अपराध वह कार्य है जिसको राज्य ने समूह के कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जिसके प्रति दंड देने की शक्ति राज्य के पास रहती है।”

प्रश्न 3.
अपराध से आप क्या समझते हैं?
उत्तर
अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो कि प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पायी जाती है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए जाते है। समाज द्वारा निर्मित इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसको समाज द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार वह कार्य, जो कानून की दृष्टि से दंडनीय होते हैं, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में, अपराध अपराधी-कानून का उल्लंघन हैं।
चाहे कोई कार्य कितना भी अनैतिक अथवा गलत क्यों न हो किंतु वह तब तक अपराध नहीं कहलाता जब तक अपराधी-कानून में उसे अपराध न माना गया हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है। कानूनी दृष्टि में अपराध वह कार्य है जो कि सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होता है। इलियट एवं मैरिल के अनुसार, “अपराध कानून द्वारा निषिद्ध (वर्जित) वह कार्य है, जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, काम-घर, सुधार-गृह या जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। अपराध सामाजिक रूप में हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए अपराध की अवहेलना करना दंडनीय है। क्लीनार्ड के अनुसार, “अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है।”
प्रश्न 4.
नगर से आप क्या समझते हैं? नगर की परिभाषा किस आधार पर की जाती है?
उत्तर
सामाजिक जीवन के संगठन के रूप में गाँव तथा नगर दोनों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। गाँव तथा नगर के मध्य कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती है। नगर की परिभाषा भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है तथा एक ही देश में भी विभिन्न जनगणना वर्षों में इसकी परिभाषा में अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड में 300 निवासियों के क्षेत्र को; अजेंटाइना में 1,000; भारत में 5,000; इटली तथा स्पेन में 10,000; अमेरिका में 20,000 तथा कोरिया गणराज्य में 40,000 निवासियों के क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। नगर के क्षेत्र के विषय में भी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं; जैसे-हंगरी के नगरों में बहुत-सा कृषि क्षेत्र सम्मिलित होता है तथा लैटिन अमेरिका में म्यूनिसिपैलिटी को बहुधा नगर मान लिया है यद्यपि इसमें बहुत-सा ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित होता है।
अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है परंतु किंग्स्ले डेविसे इससे बिलकुल सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार के वातावरण, अर्थात् नगरीय परिस्थितियों की उपज होता है। उनके अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। लुईस विर्थ ने द्वितीयक संबंधों, भूमिकाओं के खंडीकरण तथा लोगों में गतिशीलता की तेजी इत्यादि विशेषताओं के आधार पर नगर को परिभाषित करने पर बल दिया है। विर्थ के अनुसार, नगर अपेक्षाकृते एक व्यापक, घना तथा सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों का स्थायी निवास क्षेत्र होता है। विर्थ के अनुसार, जनसंख्या का आकार तथा घनत्व, विषमता तथा भिन्नता इत्यादि के आधार पर नगरीय समुदाय के लक्षण निश्चित किए जाने चाहिए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए।
उत्तर
सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोत
सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व यो सामाजिक परिवर्तन के स्रोत अग्रलिखित हैं –
1. पारिवारिक पर्यावरण – परिवार सामाजिकता की प्रथम पाठशाला है। परिवार में यदि ,शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक हो तो परिवार में संकीर्ण विचारों का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। प्रबुद्ध व्यक्ति प्राचीन परंपराओं में समयानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए जिसे समाज में प्रबुद्ध एवं शिक्षित परिवारों की संख्या अधिक होगी, उस समाज में परिवर्तन की गति भी तीव्र रहेगी। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन की गति को निर्धारित करता है।
2. मानसिक विकास – जनता के मानसिक विकास का साधने शिक्षा है। शिक्षण संस्थाओं का प्रसार जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में होगा, उस स्थान के व्यक्ति प्रबुद्ध एवं विचारशील होंगे और वे समाज में प्रचलित संकीर्णताओं व रूढ़ियों की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे, अपितु उनके स्थान पर नवीन विचारों को लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रकार, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जनता का जो मानसिक विकास होता है उसी के परिणामस्वरूप प्राचीन रीति-रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। फ्रांस जैसे देश में क्रांति को जन्म देने वाला वर्ग प्रबुद्ध वर्ग ही था। बुद्धिजीवी वर्ग ही अंसतुष्ट जनता का नेतृत्व करते हैं और प्राचीन पंरपराओं की संकीर्णता को उखाड़ फेंकते हैं।
3. समाज सुधारकों के प्रयास – प्रत्येक देश में प्राचीन परंपराओं तथा प्रथाओं में सुधार करने के लिए समाज सुधारकों के प्रयास सदैव ही जारी रहे हैं। समाज सुधारक सामाजिक कुरीतियों में परिवर्तन लाने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं तथा जनता में सामाजिक बुराइयों के विरोध में जागृति लाने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे समाज सुधारकों ने अपने अथक प्रयासों से भारत के सामाजिक जीवन के स्वरूप को बदल डाला है। ये समाज सुधारक प्रत्येक युग में अपना कार्य करते रहे हैं, अतएव सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया समाज सुधारकों के प्रयासों द्वारा निरंतर अविरल गति से चलती रहती है।
4. ज्ञान प्रसार के साधन – वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जिस समाज में समाचार-पत्रों, रेडियों, यातायात के साधनों तथा संचार-वाहने के साधनों की प्रचुरता होगी, वह समाज सामाजिक परिवर्तन का उतना ही शीघ्र स्वागत करेगा। वस्तुतः ये साधन ज्ञान-विज्ञान के विकास के साधन हैं। इन साधनों की प्रचुरता के कारण देश में नवीन विचारधाराओं को प्रसार सरलता से हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। भारत में प्राचीन मूल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन इन्हीं साधनों की देन है।
5. वैज्ञानिक आविष्कार – वैज्ञानिक आविष्कार परिवर्तन के मूल तत्त्व हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जनता का दृष्टिकोण तार्किक हो जाता है। तर्क के आधार पर प्राचीन मान्यताओं के खंडन किया जाने लगता है। इसीलिए प्राचीन रूढ़ियों व परंपराओं की मान्यता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आदान-प्रदान भी संभव हो गया है। आज भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इन वैज्ञानिक आविष्कारों की ही देन है। । ये वैज्ञानिक आविष्कार जिस तीव्र गति से होंगे, सामाजिक परिवर्तन की गति भी उतनी ही तीव्र होगी।
6. भ्रमण की स्वतंत्रता – यातायात के साधनों का विकास वैज्ञानिक आविष्कारों की देन है। इन साधनों के विकास के कारण एक देश के नागरिक दूसरे देशों में भ्रमण करके वहाँ के सामाजिक जीवन एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सामाजिक रीति-रिवाज यदि प्रगति की ओर है तो विदेशों का भ्रमण करके स्वदेश लौटे विद्वान अपने देश में विदेशी रीति-रिवाजों का प्रचार व प्रसार करते हैं और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं। जिस समय में प्रवसन की प्रवृत्ति अधिक होगी उस समाज में सामाजिक परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसलिए प्रवसन यो भ्रमण की स्वतंत्रता भी सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत है।
7. परिवर्तन की प्रवृत्ति – सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन का नाम है, साथ-ही-साथ यह संस्कृति के भौतिक तत्त्वों में भी परिवर्तन लाता है। किंतु यह सब परिवर्तन केवल उन्हीं समाजों में संभव है जिनमें नागरिक परिवर्तन को अच्छा मानते हैं या परिवर्तन की ओर नागरिकों की प्रवृत्ति है। जिस समाज में व्यक्ति परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होते हैं, उस समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। यदि समाज के व्यक्तियों में प्राचीन परंपराओं से चिपटे रहने की प्रवृत्ति पाई जाए तो सामाजिक परिवर्तन की गति मंद रहेगी। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता का अभाव इसलिए पाया जाता है कि भारतीय प्राचीन परंपराओं से चिपटने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज भी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों में उनको अटूट विश्वास है।

8. जनता में तीव्र असंतोष – जनता में प्रशासन के अत्याचारी तथा शोषण के विरुद्ध असंतोष की भावना भी सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। जब यह असंतोष की भावना तीव्रता की चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो जनता क्रांति कर बैठती है या युद्ध आरंभ हो जाते हैं। क्रांति तथा युद्ध दोनों के परिणामस्वरूप सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक हैं। नवीन एवं प्राचीन मान्यताओं में संघर्ष शुरू हो जाता है तथा प्राचीन मान्यताएँ धीरे-धीरे समाप्त होती रहती हैं और | समाज जीवन का नवीन मोड़ ले लेता है। पूँजीवाद तथा सामंतवाद के स्थान पर समाजवाद और | निरंकुशवाद के स्थान पर प्रजातंत्रवाद का जन्म जनता में तीव्र असंतोष की देन है।
9. साधनों की प्रचुरता – सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनों की प्रचुरता है। जिस देश की आर्थिक दशा अच्छी हो और उसमें प्रकृति की अनुकम्पा से खनिज पदार्थों का भी बाहुल्य हो तो वह देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होगी। उद्योग-धंधों का विकास हो जाने से जाति-पाँति के बंधन ढीले पड़ेंगे तथा संयुक्त परिवार टूटने लगेगे। इस प्रकार पारिवारिक प्रतिमानो में परिवर्तन होगा। संक्षेप में, साधनों की प्रचुरता सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है।
निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दो भिन्न परंतु परस्प संबंधित अवधारणाएँ हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक भाग है। सामाजिक परिवर्तन इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसे अनेक कारक प्रोत्साहन देते हैं तथा इसके अनेक स्रोत हैं।
प्रश्न 2.
सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
या
सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
घटनाओं की निरंतरता ही जीवन की वास्तविकता है। एक के बाद एक घटना ही मिलकर जीवन का निर्माण करती है। मानवीय जीवन के ही समान समाज के जीवन में निरंतरता एवं गतिशीलता आवश्यक तत्त्व है। गति का अभाव जड़ता का प्रतीक है। गति, वास्तव में, परिवर्तन का माध्यम होती है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में होने वाली गति सामाजिक परिवर्तन लाती है। सामाजिक परिवर्तन इस रूप में मानव समाज के विषय में मूलभूत सत्यता है।
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएँ
परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। संसार के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जब से समाज का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से समाज के रीति-रिवाज, परंपराएँ, रहन-सहन की विधियाँ, पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्थाओं आदि में निरंतर परिवर्तन होता आया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही वैदिक काल के समाज में और वर्तमान समाज में आकाश-पाताल का अंतर पाया जाता है। परंतु यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं होता वरन् केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। प्रमुख विद्वानों ने इसे अग्र प्रकार से परिभाषित किया है –
1. जॉन्स (Jones) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंत:क्रिया या सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।”
2. मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार – “समाजशास्त्री होने के नाते हमारी । प्रत्यक्ष रुचि सामाजिक संबंधों में हैं। हम केवल उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इनमें (अर्थात् सामाजिक संबंधों में) होते हैं।”
3. जॉनसन (Johnson) के अनुसार -“सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है।”
4. जेनसन (Jenson) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीको में होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।”
5. डेविस (Davis) के अनुसार – “सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात् समाज के ढाँचे और कार्यों में घटित होते हैं।”
6. डॉसन एवं गेटिस (Dawson and Gettys) के अनुसार – “सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक है।”
7. फिचर (Fichter) के अनुसार – “संक्षेपत: पहले की अवस्था या रहन-सहन के ढंग में भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं।”
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का संबंध सामाजिक संबंधों तथा समाज की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। कालांतर में सामाजिक संबंधी तथा समाज की संरचना और प्रकायों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज से है तथा प्राकृतिक या जैविक जगत् में होने वाले परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं है।
सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएँ
सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं से इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं –
1. सर्वव्यापकता – सामाजिक परिवर्तन मानव समाज के इतिहास के आरंभ से अब तक सभी कालों में होता चला आ रहा है। इतिहास का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा जिसने मानव समाज को कोई-न-कोई नई विचारधारा प्रदान न की हो। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव समाज में सभी स्थानों पर किसी-न-किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन अवश्य होता आ रहा है।
2. सापेक्ष गति – सामाजिक परिवर्तन की गति को हम एक समाज में होने वाले परिवर्तनों की दूसरे समाजों में होने वाले परिवर्तन से तुलना करके ही निश्चित कर सकते हैं। एक-सी परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर भी सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि सभी समाज परिवर्तन की दशाओं, से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। ग्रामीण समाज में नगरीय समाज की अपेक्षा परिवर्तन की गति धीमी होती है। हम विभिन्न समाजों में होने वाले परिवर्तनों को देखकर यह कह सकते हैं कि किस समाज में कितना परिवर्तन हुआ है। इसलिए विद्वानों का मत है कि सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्ष होती है।
3. एक जटिल प्रक्रिया – सामाजिक परिवर्तन का संबंध सदैव गुणात्मक परिवर्तन से होता है। गुणात्मक परिवर्तन का कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतएव सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य या प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन सदैव ही दो प्रकार के तत्त्वों को प्रभावित करता है। जब यह भौतिक तत्त्वों को प्रभावित करता है तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि हमारे आविष्कारों में कितना परिवर्तनन हुआ है, किंतु जब हमारे सांस्कृतिक तत्त्वों में परिवर्तन होता है तो वह इतना धीमा होता है कि उसको समझना सरल नहीं होता और तब हम उस परिवर्तन को जटिल प्रक्रिया के. नाम से पुकारते हैं।
4. भविष्यवाणी का अभाव – सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं में परिवर्तन होता है, किंतु सामाजिक परिवर्तन के संबंध में यह कहना कठिन है कि कौन-से कारणों द्वारा कितना परिवर्तन किस समाज में होगा। हम किसी समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कल्पना मात्र कर सकते हैं, यह नहीं कह सकते है कि समाज पर औद्योगीकरण, नगरीकरण आदि तत्त्वों का किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा और यह भी नहीं कह सकते कि समाज में प्रचलित परंपराओं तथा प्रथाओं का प्रभाव किस सीमा तक कम हो जाएगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों के स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा। साथ ही, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है।
5. अनिवार्यता – सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है जो प्रत्येक समाज में होती रहती है। सभी व्यक्तियों के उद्देश्य एवं विचार समान नहीं होते। सभी व्यक्ति अपने-अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयास में वे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। और विचार-विर्मश के कारण नई बातों या नए विचारों को जन्म देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसलिए ए० डब्ल्यू० ग्रीन (A. W. Green) ने भी कहा है-“परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत अपने जीवन का प्रायः एक ढंगे-सा बन चुका है।”
6. अन्य विशेषताएँ – विल्बर्ट ई० मूर (Wilbert E. Moore) ने सामाजिक परिवर्तन की कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिलाया है –
- सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से होता है।
- सामाजिक परिवर्तन की गति आधुनिक युग में अपेक्षाकृत तीव्र है।
- सामाजिक परिवर्तन हमारे भौतिक जीवन को तीव्र गति से प्रभावित करता है। इसलिए | आज भोजन व वस्त्रों में पहले से अधिक अंतर आ गया है। हम आज आकर्षक तथा भोग-विलास की वस्तुओं से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं।
- सामाजिक परिवर्तन हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर धीमी गति से प्रभाव डालता है।
- जो परिवर्तन हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है उसकी गति अधिक तीव्र होती है।
- सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत अवधारणा है। इसका अभिप्राय सामाजिक संबंधों तथा समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ-साथ विभिन्न समाजों में असमान गति से निरंतर होता रहता है।

प्रश्न 3.
सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमानों की विवेचना कीजिए।
उत्तर
सामाजिक परिवर्तन के विस्तृत प्रतिमान
सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत संप्रत्यय है जिसका कोई एक निश्चित प्रतिमान नहीं है। मुख्य प्रश्न हमारे सामने यह है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए किस कारक को आधार माना जाए तो और व्याख्या करने में कौन-सी पद्धति को अपनाया जाए? विद्वानों ने इस समस्या को निमनलिखित दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया है –
1. अन्योन्याश्रितता एवं कारकों की विविधता – जब हम समाज में होने वाले किसी भी परिवर्तन को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उसके एक नहीं बल्कि अनेक कारक हैं जो कि परस्पर भिन्न न होकर अन्योन्याश्रित है अर्थात् ये एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए मनोधारणाओं या मनोवृत्तियों में परिवर्तन तथा मानव मनोवृत्तियों पर उसके संपूर्ण पर्यावरण एवं दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए आर्थिक दशाओं तथा प्रौद्योगिकीय एवं राजनीतिक पक्षों से भी परिचित होना । पड़ता है।
कुछ परिवर्तन इसलिए होते रहते हैं कि हम भौतिक पर्यावरण से सांमजस्य स्थापित कर सकें। उदाहरणार्थ-यदि हम गिरती हुई जन्म-दर का अध्ययन करें तो हमें धार्मिकता, महिलाओं की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, देर से विवाह, व्यक्तिवाद आदि का अध्ययन करना ही होगा। इस संयुक्त योगदान को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता; अतः बाध्य होकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में हमें विविध कारकों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा किए बिना हम सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझ सकते। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने से हम किसी एक कारक को निर्णायक कारक मानकर नहीं चल सकते।
समाज में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारक आपस में अंतसंबंधित हैं। यही कारण है कि वे स्वयं पूर्ण न होकर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। किसी सामाजिक घटना का वर्णन करते समय न केवल कारकों की बहुलता या विविधता ही ध्यान में रखती है वरन् उनकी अंतर्निर्भरता को भी उतनी ही महत्ता देनी होगी। विविध कारण एक-दूसरे से मिले और गुंथे रहते हैं। अपराधों में वृद्धि का कारण हम व्यक्तिवाद को मानते हैं जिसने व्यक्ति को संयुक्त परिवार से अलग किया और संयुक्त परिवार का ह्वास करके एकाकी परिवार बसाने को प्रोत्साहित किया। अपराधों में वृद्धि का दूसरा कारक नगरीकरण माना जाता हैं क्योंकि जीविकोपार्जन हेतु गाँवों के लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ की गन्दी बस्तियो के वातावरण में अपराध करने के अधिक अवसर मिलने पर अपराधों में भाग लेने लगते हैं। यहाँ उन्हें जनसंख्या में विविधता मिलती है।
जिससे अपराध करके भीड़भाड़पूर्ण वातावरण में छिपने की सुविधा, औद्योगिक केंद्रों में अपराधी व्यक्ति को खोज पाने की कठिनाई तथा साथ ही तीव्रगामी आवागमन के साधनों में वृद्धि के कारण एक स्थान पर अपराध करके दूसरे स्थान पर आसानी से भाग जाने की सुविधा आदि संभव होने के कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है। अपराध का तीसरा कारक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोरी है। ऐसे व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे अपराध एवं उससे समाज को होने वाली हानि तथा अपने पर इसके होने वाले दुष्प्रभावों के विषय के बारे में सोच सकें। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता का शिकार होने के कारण निराश हो और इसी कारण अपराध करता हो।
अब यह प्रश्न उठता है कि क्या वे सब कारक एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं? क्या व्यक्तिवाद नगरीकरण का ही परिणाम है? क्या नगरीकरण औद्योगीकरण का ही शिशु नहीं है? क्या आवागमन के साधनों में वृद्धि, नगरीकरण, व्यक्तिवाद, द्वितीयक समूहों का विकास तथा अपराध वृद्धि आदि सभी कारक पारस्परिक निर्भरता की कड़ी में नहीं बँधे हैं? समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कारक स्वतंत्र कारक नहीं बल्कि एक-दूसरे के साथ सहयोगी व्यवस्था में बँधकर किसी सामाजिक व्यवहार को जन्म देते हैं। सामाजिक कारक आपस में तार्किक रूप से कार्य-कारण संबंधों से भी जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार; यह प्रमाणित हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में कारकों की | विविधता तथा उनकी अन्योन्याश्रितता को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।
2. परिमाणात्मक पद्धति की असमर्थता – कुछ विद्वान यह विश्वास करते हैं कि हर सामाजिक घटना का अध्ययन हम परिणात्मक सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। उदाहरणार्थअपराधों का अध्ययन करने के लिए हम संयुक्त परिवार के विघटन पर भी दृष्टिपात करते हैं। कितने संयुक्त परिवार विघटित हुए यह जानने के लिए हम संयुक्त परिवार के विघटने पर भी दृष्टिपात करते हैं। कितने संयुक्त परिवार विघटित हुए यह जानने के लिए हमें उनकी संख्या गिननी होगी जिसमें इस पद्धति का सहारा लेना होगा। परंतु सामाजिक संबंधों का एक परिमाणात्मक पहलू भी है जो अति न्यून है। भौतिक विज्ञानों के समान परिमाणात्मक पद्धति को यदि हम समाजशास्त्र में भी लागू करते हैं तो बड़ा भय उपस्थित हो जाता है। सामाजिक घटनाओं में प्राकृतिक घटनाओं के समान किसी परिस्थिति में से अलग किए जा सकने वाला।
कोई भाग नहीं होता है। विभिन्न भाग अपने संदर्भ में अलग होते ही अर्थहीन हो जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं क्योंकि ने तो उनका कोई भौतिक स्वरूप होता है और न ही आकार। अतः उन्हें रेखागणितीय या परिमाणात्मक पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। साथ ही, यदि एक घटना को पैदा करने में कई कारकों का योगदान रहता है। तो उनमें से प्रत्येक कारक का कितना अलग-अलग व्यक्तिगत योगदान है, यह ज्ञात करना अति कठिन है।
उपर्युक्त दोनों परिप्रेक्ष्यों के कारण सामाजिक परिवर्तन के विस्तृत प्रतिमान के निर्धारण की समस्या और अधिक उलझ जाती है। इन समस्याओं के बावजूद समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख विस्तृत प्रतिमानों को समझने में काफी सीमा तक सफल रहे हैं।
सामाजिक परिवर्तन समस्त समाजों में एक-सा नहीं हो सकता; अत: हमें परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान दृष्टिगोचर होते हैं। यदि किंही दो समाजों में परिवर्तन के समान कारक कार्य कर रहे हों तो भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उन दोनों समाजों में परिवर्तन के प्रतिमान भी समान ही विकसित होंगे, क्योंकि परिवर्तन से कारकों का क्रमागत एकीकरण (Orderly integration) भी समान होगा यह आवश्यक नहीं है। इसी से दो भिन्न समाजों में परिवर्तन के एक से ही कारकों के कार्यरत रहने पर प्रतिमान भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के अनेक प्रतिमान देखे जा . सकते हैं तथापि मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित तीन प्रतिमान हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं –
1. पहला प्रतिमान : रेखीय परिवर्तन – सामाजिक परिवर्तन के प्रथम प्रतिमान के अनुसार परिवर्तन यकायक होता है और फिर क्रमश: मंदगति से अनिश्चितकाल तक सदैव ऊपर की ओर होता रहता है। अतः यह परिवर्तन उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है। परिवर्तन की यह रेखा सदैव ऊपर की ओर चलती रहती है। उदाहरणार्थ-हम आवागमन एवं संदेशवाहन के साधनों को ले सकते हैं। एक बार जब कोई आविष्कार हो जाता है तो उत्तरोत्तर ऊपर चला जाता है तथा अन्य अनेक नवीन आविष्कारों का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन भी इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार विज्ञान में होने वाले परिवर्तन भी इससे बहुत-कुछ साम्य रखते हैं। अतः निरंतर उन्नत होते प्रतिमान रेखीय प्रतिमान कहलाते हैं। इनकी उन्नति की गति तीव्र भी हो सकती है और मंद भी। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “वास्तव में, इस प्रकार के परिवर्तन की विशेषता उसकी यकायक में नहीं बल्कि एक उपयोगी व्यवस्था के निरंतर संचयी विकास के रूप में है जब तक कि इस व्यवस्था को उसी भाँति उत्पन्न कोई दूसरी नई व्यवस्था अचानक आकर जड़ से ही न उखाड़ फेंके।”
2. दूसरा प्रतिमान : उन्नति – अवनतिशील परिवर्तन – परिवर्तन के इस प्रतिमान के अनुसार परिवर्तन एवं विकास क्रमशः नहीं होता है वरन् एक ही स्थिति के बिलकुल विपरीत स्थिति भी तुरंत ही परिवर्तित हो जाती है। कुछ समय तक परिवर्तन का प्रवाह लगातार ऊपर की दिशा में जाता है, बाद में यह एकदम विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और अवनति के ये सोपान परिलक्षित होते रहते हैं। आर्थिक जगत तथा जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन इसी प्रतिमान की अभिव्यक्ति करते हैं। आर्थिक जगत में सामान्यतः अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जनसंख्या भी बढ़ती जाती है और फिर एकदम से घटनी शुरू हो जाती है। प्रथम प्रतिमान (रेखीय परिवर्तन) में यह निश्चित है कि परिवर्तन निश्चित दिशा में सदैव ऊर्ध्वगामी होता है, किंतु इस द्वितीय प्रतिमान में कुछ पता नहीं रहता कि परिवर्तन कब अपनी विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाएगा जो चरमोन्नत से निम्नतम और निम्नतम से चरमोन्नत कुछ भी हो सकता है।
3. तीसरा प्रतिमान : चक्रीय परिवर्तन – परिवर्तन का यह प्रतिमान दूसरे प्रतिमान से काफी मिलता-जुलता है। यह परिवर्तन पूरे जीवन अथवा उसके कई भागों में उसी प्रकार से देखने में आता है जैसे कि प्राकृतिक जगत में। इसकी तुलना साइकिल के पहिए की भाँति चलने वाले चक्र से की जा सकती है। प्राकृतिक जगत में इस प्रकार के परिवर्तन देखने में आते हैं। मौसमों में होने वाला क्रमशः चक्रीय परिवर्तन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे समुद्र अथवा नदी में एक के पीछे दूसरी लहरें उठती रहती हैं और उस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार परिवर्तन आदि-अंत विहीन निरंतर होता रहता है। यह चक्र मानव जीवन में भी देखा जा सकता है। मनुष्य का जन्म होता है, वह युवा होता है, वृद्ध होता है तथा मर जाता है। ये अवस्थाएँ अवश्यम्भावी है। फैशन में होने वाले परिवर्तन तथा रूढ़ियों में होने वाले परिवर्तन इसी प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक विकास में भी कई बार इसी प्रतिमान को देखा जा सकता है।
इस प्रकार यद्यपि हम उपर्युक्त प्रतिमानों को व्यक्त करते हैं तथापि सभी परिवर्तनों को इन तीन प्रतिमानों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। कुछ परिवर्ततन ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों में किसी भी प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आते हैं अथवा तीनों में ही आते हैं। वस्तुतः मानव संबंधों को अधिकतर भाग गुणात्मक है; अतः जब किसी परिवर्तन में सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश होता है तो हमारे लिए उस परिवर्तन को किसी एक प्रतिमान के अंतर्गत रखना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई के बावजूद अधिकांश समाजशास्त्री सैद्धांतिक रूप में सामाजिक परिवर्तन के उपर्युक्त तीनों प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं।
प्रश्न 4.
सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन-से हैं?
या
सामाजित परिवर्तन के विभिन्न कारकों को संक्षेप में बताइए।
या
सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। आपकी दृष्टि से भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन-सा कारक अधिक महत्त्वपूर्ण है और क्यों?
उत्तर
सामाजिक परिवर्तन के कारक
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के विभिन्न पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है। इसे अनेक कारण या कारक प्रोत्साहन देते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले मुख्य कारकों का संक्षिप्त परिचय निम्नवर्णित है –
1. जैविक कारक – मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन के दूसरे साधन, सामाजिक निरंतरता को जैविक दशा में, जनसंख्या के बढ़ाव व घटाव तथा प्राणियों व मनुष्यों की वंशानुगत दशा के ऊपर निर्भर हैं। जैविक कारकों से तात्पर्य जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष से है जो कि वंशानुगत के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। हमारी शारीरिक व मानसिक क्षमताएँ, स्वास्थ्य व प्रजनन दर वंशानुक्रमण व जैविक कारकों से प्रभावित होते हैं। जैवकीय कारक अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। वंशगंत मिश्रण को रोका नहीं जा सकता। इस कारण ही प्रत्येक पीढ़ी में शारीरिक अंतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रवरण और अस्तित्व के लिए संघर्ष के जैवकीय सिद्धांत भी समाज में बराबर परिवर्तन करते रहते हैं।
2. भौतिक या भौगोलिक कारक – सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में भौतिक या भौगोलिक तत्त्वों या परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है। संसार की भौगोलिक परिस्थितियों में दिन-रांत परिवर्तन हो रहा है। तीव्र वर्षा, तूफान, भूकंप आदि पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन करते आए हैं जिनका मनुष्य की सामाजिक दशाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता आया है। हटिंगटन के मतानुसार, जलवायु का परिवर्तन ही सभ्यताओं और संस्कृति के उत्थान एवं पतन को एकमात्र कारण है। जिस स्थान पर लोहा और कोयला निकल आता है, वहाँ के समाज में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। भले ही इस कथन में पूर्ण सत्यता न हो परंतु पर्याप्त सीमा तक सत्यता अवश्य है।
3. मनोवैज्ञानिक कारक – सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में मनोवैज्ञानिक कारकों का विशेष हाथ रहता हैं। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदा नवीन खोजे किया करता है और नवीन अनुभवों के प्रति इच्छित रहता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप ही मानव समाज की रूढ़ियों, परंपराओं तथा रीति-रिवाजों में परिवर्तन होते. रहते हैं। मानसिक असंतोष तथा मानसिक संघर्ष व तनाव सामाजिक संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा इनसे हत्या, आत्महत्या, अपराध, बाल अपराध, पारिवारिक विघटन आदि को प्रोत्साहन मिलता है।
4. प्रौद्योगिकीय कारक – सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकीय कारक विशेष भूमिका रहती है; ऑगबर्न (Ogburn) के शब्दों में, “प्रौद्योगिकी हमारे वातावरण को परिवर्तित करके, जिससे कि हम अनुकूलन करते हैं, हमारे समाज को परिवर्तित करती है। यह परिवर्तन सामान्य रूप से भौतिक पर्यावरण में होता है और हम परिवर्तनों से जो अनुकूलन करते हैं उससे बहुधा प्रथाएँ और सामाजिक संस्थाएँ संशोधित हो जाती है। वास्तव में, विभिन्न आविष्कारों और औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज हमारे रहन-सहन, खान-पान तथा आपसी संबंधों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनका मूल कारण औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास के कारण गृह उद्योग-धंधे बंद हो गए, समाज में बेकारी और भुखमरी का बोलबाला हो गया।
संक्षेप में, औद्योगिक विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव नगरीकरण, श्रम संगठन, विशेषीकरण, बेकारी तथा प्रतियोगिता आदि के रूप में देखा जा सकता है कि प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं तथा इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। वैबलन (Vablen) ने सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख कारक माना है। प्रौद्योगिकी श्रम संगठनों, नगरीकरण, गतिशीलता, विशेषीकरण तथा सामाजिक संबंधों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व पारिवारिक जीवन पर इसके अनगिनत अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। वैबलन के अनुसार, प्रौद्योगिकी का सर्वप्रमुख प्रभाव हमारी आदतों पर पड़ता है और आदतों से विचारों का निर्माण होता है। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन से आदतों व विचारों में परिवर्तन हो जाता है; अत: प्रौद्योगिकी ही यह निर्धारित करती है कि हमारा सामाजिक ढाँचा तथा हमारी संस्थाएँ कैसी होंगी।
5. जनसंख्यात्मक कारक – जनसंख्या में परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के घटने-बढ़ने का देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता हैं जिन देशों में प्राकृतिक स्रोत तो कम होते हैं, परंतु जनसंख्या अधिक होती है वहाँ निर्धनता और भुखमरी का बोलबाला रहता है। जहाँ अनुकूल व आदर्श जनसंख्या होती है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है। इसके साथ ही जन्म व मृत्यु दर भी परिवर्तन लाती हैं। अगर मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या कम होती जाती है तथा अधिक बच्चों के जन्म को प्राथमिकता देने वाली प्रथाएँ विकसित होने लगती हैं। अगर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाती है जिससे निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी आदि में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में गतिशीलता (आप्रवासे तथा उत्प्रवास), जनसंख्या में औसत आयु तथा लिंग अनुपात:कुछ अन्य जनसंख्यात्मक कारक है जो कि सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक हैं। जनंसख्या के विकास के साथ-साथ सामाजिक मान्यताओं, प्रथाओं और रीति-रिवाजों में भी परिवर्तन आता है।
6. आर्थिक कारक – सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। माक्र्स ने आर्थिक कारकों को निर्णायक कारक बताया है। वर्ग-संघर्ष आर्थिक कारणों के परिणामस्वरूप ही विकसित होता है। उत्पादन के स्वरूपों, संपत्ति के स्वरूपों, व्यवसायों की प्रकृति, वितरण प्रणाली, औद्योगीकरण, श्रम-विभाजन तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अतः इनमें परिवर्तन होने पर सामजिक परिवर्तन को . प्रोत्साहन मिलता है। माक्र्स के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया एक ऐसे वर्ग को विकसित करती है जो कि उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। यह वर्ग पूँजीपति वर्ग कहलाता है। पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करके श्रमिकों को उत्पादन कार्य में नियोजित करता है। श्रमिक वस्तुओं के उत्पादन में अपना श्रम लगाते हैं और उत्पादित वस्तुओं का अधिकांश लोभ (अतिरिक्त मूल्य) पूँजीपति वर्ग ही हड़प जाता है। श्रमिकों के इस शोषण से उनमें असंतोष पैदा होता है तथा वे संगठित होकर पूँजीपति वर्ग से संघर्ष करते हैं। इसी वर्ग-संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन आता है। माक्र्स के अनुसार हमारी सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचा, विचार इत्यादि सभी आर्थिक कारकों से प्रभावित होते है।
7. सांस्कृतिक कारक – सांस्कृतिक कारक का सर्वाधिक पक्ष मैक्स वेबर (Max Weber), सोरोकिन (Sorokin) तथा ऑगबर्न (Ogburn) ने लिया है। मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्मों और व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होने के कारण समाज में परिवर्तन होते हैं। सोरोकिन ने सांस्कृतिक उतार-चढ़ाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दी है। किस सीमा तक यह सत्य भी है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन आने से सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं; जैसे–पर्दा प्रथा की समाप्ति, स्त्री-शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों को नौकरी करना, संयुक्त परिवार का विघटन और जाति प्रथा का विरोध आदि।
निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है। इसे अनेक कारक प्रोत्साहन देते हैं तथा कई बार यह विविध प्रकार के कारकों का सामूहिक परिणाम होता है। यही कारक भारत में भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।
प्रश्न 5.
सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं? इस व्यवस्था को विस्तार से समझाइए।
या
सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा को बताते हुये सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर
सामाजिक जीवन मानवों के मध्य होने वाली अंत:क्रियाओं का एक सतत एवं निरंतर प्रवाह है। मानवीय अंत:क्रियाएँ मनमाने ढंग से घटित नहीं होती अपितु अधिकांशतः वे सुनिश्चित व पूर्व-निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार घटित होती हैं। इसी से समाज में स्थायित्व, निरंतरता और व्यवस्था बनी रहती है। ‘सामाजिक व्यवस्था’ का अर्थ समझने के लिए पहले व्यवस्था’ शब्द का अर्थ समझ लेना अनिवार्य है। ‘व्यवस्था’ शब्द से किसी वस्तु अथवा समग्र के विभिन्न धारकों या अंगों का तथा उनमें पाए जाने वाले संबंधों का बोध होता है।
व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषाएँ
कंसाइज ऑक्सफोर्ड शब्दकोश’ (Concise Oxford Dictionary) में व्यवस्था’ शब्द का प्रयोग दो भिन्न संदर्भो में किया गया है – प्रथम, व्यवस्था एवं जटिल समग्र या संबंधित वस्तुओं तथा घटकों का कुलक या भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं का संगठित निकाय है तथा द्वितीय, व्यवस्था से प्रणाली, संगठन तथा कार्य-पद्धति और वर्गीकरण के निर्धारित सिद्धांत का बोध होता है।
उपर्युक्त दोनों अर्थों में संबंधित, संगठित तथा संगठन महत्त्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि व्यवस्था एक ऐसा कुलक है जो संगठित है अथवा जिसके विभिन्न घटक परस्पर संबद्ध हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसे समाकलित समग्र (Integrated whole) अथवा कुलक से हैं जिसके विभिन्न घटक परस्पर संबंधित तथा संगठित होते हैं।
‘व्यवस्था’ शब्द की परिभाषा करते हुए विलबर आम (Wilbur Schramm) ने लिखा है-“जब कभी हम एक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा आशय अन्योन्याश्रित कणों के एक ऐसे समुच्चय या कुलक (सेट) से होता है जो सीमाओं को बनाए हुए हैं।”
इस परिभाषा में दो महत्त्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है – एक तो ‘अन्योन्याश्रितता’ तथा दूसरा ‘सीमाएँ। अन्योन्याश्रितता से आशय यह है कि किसी व्यवस्था की संघटक इकाइयों एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि इसके किसी भी हिस्से में होने वाली कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म हो, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जहाँ तक सीमाओं को बनाए रखने का प्रश्न है, इससे यह तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवस्था की एक स्पष्ट सीमा रेखा भी दिखाई देती हैं यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहाँ इस व्यवस्था का कार्य-क्षेत्र प्रारंभ होता हैं और कहाँ यह समाप्त होता है। उदाहरण के लिए हम एक कॉलेज को लें। कॉलेज की एक व्यवस्था के रूप में कल्पना की जा सकती है और इस रूप में उसका विवेचन भी संभव है। कॉलेज में विभिन्न कक्षा-समूह, विषयानुसार शिक्षकों के अनेक विभाग, कार्यालय-कर्मचारी, प्रबंध-समिति आदि अनेक इकाइयाँ परस्पर प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी हुई कॉलेज की व्यवस्था का निर्माण करती हैं।
इनमें से किसी एक इकाई में घटित घटना कॉलेज में सभी हिस्सों को प्रभावित करेगी अर्थात् पूरी कॉलेज व्यवस्था उससे प्रभावित होगी। यह भी सच है कि कॉलेज शून्य में कोई कार्य नहीं करता। उसके चारों ओर विद्यमान समुदाय, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। कॉलेज भी इन अन्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, परंतु वे अन्य सभी क्वस्थाएँ कॉलेज के सामाजिक पर्यावरण को प्रकट करती है। इस समस्त सामाजिक पर्यावरण में कॉलेज के पर्यावरण की सीमाएँ कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं – यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, सीमांकित किया जा सकता है। इसी प्रकार हाल एवं फेगन (Hall and Fagen) ‘व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखते हैं-“किन्हीं भी चीजों का एक समुच्य, जहाँ उन चीजों के बीच और उन चीजों के गुणों के बीच संबंध हो, व्यवस्था कहलाता है।”
इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न इकाइयों के बीच अंत:संबंध ही व्यवस्था का मूल आधार है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि किन्हीं इकाइयों का योग मात्र या ढेर, व्यवस्था नहीं है। वे इकाइयाँ जब एक विशेष ढंग से अंत:संबंधित हो जाती हैं तो एक पृथक् अस्तित्व, एक समग्रता का प्रादुर्भाव होता है जो उन इकाइयों के योग से बिलकुल अलग है। यह समग्रता (Wholeness) ही व्यवस्था की परिचायक है। यही तथ्य इस सर्वविदित सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट होता है। कि “समग्र इकाइयों के योग से बड़ा होता है।”
उदाहरण के लिए हम कॉलेज व्यवस्था को विद्यार्थियों की संख्या, कुर्मचारियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या और प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या का योग मात्र नहीं कह सकते। वह तो इन सब इकाइयों के बीच संबंधों की व्यवस्था का नाम है। ठीक ऐसे ही जैसे-ईंट, पत्थर, गारा, चूने का योग या एक जगह ढेर मकान नहीं कहा जा सकता।
सामाजिक व्यवस्था का अर्थ तथा परिभाषाएँ
अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। ऐसे विद्वानों का संप्रदाय संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक संप्रदाय कहलाता है। ऐसे विद्वानों का मत है कि समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है और उसके जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं घटनाओं का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अतः यद्यपि अधिकांश विद्वान व्यक्ति तथा व्यक्तियों में पाए जाने वाले संबंधों को सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई मानते है, फिर भी कुछ विद्वान समूह एवं समाज के स्तर पर सामाजिक वास्तविकता की बात करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा द्वारा हम वास्तविकता को व्यक्त करते हैं।
सरल शब्दों में, सामाजिक व्यवस्था को परस्पर अंत:क्रियारत व्यक्तियों अथवा समूहों का कुलक (Set) कहा जा सकता है। यह ऐसा कुक्क है जिसे सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता है एवं जिसका व्यक्तियों (जो इस कुलके का निर्माण करते हैं) से भिन्न अपना पृथक् अस्तित्व है। प्रमुख विद्वानों ने सामाजिक व्यवस्था की परिभाषाएँ निम्न प्रकार से देने का प्रयास किया है –
1. सोरोकिन (Sorokin) के अनुसार – सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था की परिभाषा “अभिप्रायों | की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में दे सकते हैं जिसमें शब्दों द्वारा संचारित होने की क्षमता है तथा
जो अंत:क्रियाओं के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के समान प्रतीत होती है।”
2. पेरेटो (Pareto) के अनुसार – समाज विभिन्न शक्तियों के साम्य की एक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था समाज की वह अवस्था है जो किसी दिए हुए समय तथा परिवर्तन की उत्तरोत्तर दशाओं से प्राप्त होती है।”
3. टालकट पारसंस (Talcott Parsons) के अनुसार – “सामाजिक व्यवस्था में वैयक्तिक कर्ताओं की बहुलता होती है, जो एक ऐसी स्थिति में एक-दूसरे से अंत:क्रियाएँ करते हैं जिनका कम-से-कम एक भौतिक अथवा पर्यावरण संबंधी पहलू होता है। इस व्यवस्था के कर्ता अत्यधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की भावना से प्रेरित होते हैं और अंत:क्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, जिनमें परिस्थितियों के साथ उनके संबंध भी सम्मिलित हैं, सांस्कृतिक रूप से संचारित तथा स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित एवं व्यवस्थित होते हैं।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण एक से अधिक वयैक्तिक कर्ताओं की पारस्परिक अंतक्रियाओं से होता है। यह अंत:क्रियारत व्यक्तियों अथवा समूहों की कुलक है जिसका सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्तियों से भिन्न अपना पृथक् अस्तित्व होता है।
सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ
यद्यपि पेरेटो एवं सोरोकिन ने भी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट किया है फिर भी इस अवधारणा को विकसित करने में टालकट पारसंस को विशेष योगदान रहा। इन विद्वानों के विचारों से सामाजिक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं –
1. अर्थपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाएँ – व्यक्ति की प्रत्येक प्रकार की क्रियाएँ तथा अंतःक्रियाएँ सामाजिक व्यवस्था को विकसित नहीं करती अपितु केवल विभिन्न प्रस्थितियों वाले व्यक्तियों की अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं, जो कि उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के परिणामस्वरूप होती हैं, के संगठित रूप द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संबंधों पर आधारित क्रियाओं एवं अंत:क्रियाओं के संयोग एवं क्रमबद्ध रूप को ही सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
2. एकता एवं क्रम – सामाजिक व्यवस्था केवल व्यक्तियों के संयोग अथवा अंगों के संकलन को ही नहीं कहते, अपितु व्यक्तियों की अंत:क्रियाओं अथवा विभिन्न अंगों में एक निश्चित क्रम तथा एकता का होना सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य दशा है।
3. व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता – सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अंत:क्रिया में लगे हुए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा होता है। यह इसके निर्माण की प्रथम अनिवार्य विशेषता है। अनेक व्यक्तियों की क्रियाओं तथा अंतक्रियाओं द्वारा सामाजिक व्यवस्था विकसित होती है, न कि किसी एक व्यक्ति की क्रिया द्वारा।
4. समाकलित समग्र – सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग प्रकार्यात्मक संबंधों द्वारा एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि एक अंग में परिवर्तन अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है तथा इसीलिए इसे समाकलित समग्र कहा गया है। इससे हमें यह भी पता | चलता है कि व्यवस्था स्थिर न होकर गतिशील होती है।

5. सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित – पारसंस ने तीन प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है –
(i) व्यक्तित्व व्यवस्था
(ii) सामाजिक व्यवस्था तथा
(iii) सांस्कृतिक व्यवस्था।
सामाजिक व्यवस्था का स्तर व्यक्तित्व व्यवस्था से तो विस्तृत हैं परंतु सांस्कृतिक व्यवस्था से सीमित है। वास्तव में, सांस्कृतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है, जबकि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं और अंत:क्रियाओं को निर्धारित करके व्यक्तित्व व्यवस्था को प्रभावित करती है। संस्कृति ही सामाजिक व्यवस्था के अंगों को प्रकार्यात्मक रूप से जोड़ने और सामाजिक व्यवस्था के तनाव को कम करने का कार्य करती है।
6. भौतिक तथा पर्यावरण संबंधी पहलू – सामाजिक व्यवस्था किसी शून्य में कार्य नहीं करती अपितु इसका एक भौतिक एवं पर्यावरण संबंधी पहलू होता है। सामाजिक व्यवस्था को किसी निश्चित क्षेत्र, समय तथा समाज के संदर्भ में ही समझा जा सकता है अर्थात् प्रत्येक समाज में तथा इतिहास के विभिन्न युगों में अथवा किन्हीं दो समाजों ने एक-सी सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है। भौतिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण में परिवर्तन होने के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहते हैं।
7. अनुकूलन – सामाजिक व्यवस्था में पर्यावरण के परिवर्तित होने अथवा अंगों के कार्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है अर्थात् यह परिवर्तित परिस्थिति से अनुकूलन कर लेती है। अंगों तथा इकाइयों में परिवर्तन के बावजूद अनुकूलन द्वारा समग्र में निरंतरता बनी रहती है तथा सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था के रूप में कार्यरत रहती है।
8. परिस्थितियाँ एवं लक्ष्य – सामाजिक व्यवस्था एक लक्ष्य-निर्देशित क्रिया होती है तथा लक्ष्य परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था विभिन्न परिस्थितियों से व्यक्तियों का अनुकूलन करने तथा उनकी आवश्यकता एवं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायता देती है।
9. सीमाएँ – सामाजिक व्यवस्था को किन्हीं निश्चित सीमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सीमाओं के आधार पर ही इसे सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक व्यवस्था से पृथक् किया जा सकता है।
10. संतुलन तथा व्यवस्था – सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाले अंगों में निश्चित क्रम अथवा व्यवस्था तथा संतुलन पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन की इसी विशेषता के
कारण यह एक गतिशीलता के रूप में कार्यरत है।
11. सामाजिक व्यवस्था की संपूर्णता – सामाजिक व्यवस्था का एक सामाजिक इकाई के रूप में , पृथक् अस्तित्व होता है। जब भी हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय संपूर्णता या समग्रता से होता है। इसीलिए यह अंगों का योग मात्र नहीं है।
प्रश्न 6.
भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए।
या
भारत में सामाजिक परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर
भारतीय में सामाजिक परिवर्तन की दिशाएँ
भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रगति धीमी रही है किंतु फिर भी भारतीय समाज परिवर्तन की दिशा में सदैव आगे बढ़ रहा है। भारतीय समाज में इस प्रकार का परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं –
(क) सामाजिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन
भारतीय सामाजिक संस्थाओं में विवाह तथा परिवार दो प्रमुख संस्थाएँ हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इन दोनों सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया है। इनमें होने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं –
1. लघु परिवारों पर बल – परिवार के सदस्यों की संख्या को कम करने पर बल दिया जाता है। ‘छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत में विश्वास किया जाने लगा है। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार तो लेते ही जा रहे हैं साथ ही संयुक्त परिवारों का आकार भी छोटा होता जा रहा है।
2. परिवार नियोजन – परिवार में जनसंख्या की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन लागू कर दिया गया है। आज बच्चों को भगवान की देन नहीं माना जाता है। इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन
पश्चिमीकरण एवं लौकिकीकरण के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाया है।
3. एकाकी परिवारों का जन्म – परिवार के आकार में परिवर्तन हो गया है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं तथा इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
4. पारिवारिक विघटन – स्त्रियों को स्वतंत्रता, घर के बाहर नौकरी करने की सुविधा तथा उत्तराधिकार अधिनियम् पारित हो जाने के कारण स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है, किंतु
पारिवारिक विघटन आरंभ हो गया है।
5. स्त्रियों की आत्मनिर्भरता – परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन होने लगे हैं। स्त्रियों की शिक्षा तथा उनकी आत्मनिर्भरता के कारण स्त्रियों में संतोषजनक रूप से सुधार हुआ है तथा कुछ ‘ लोगों का कहना है कि इससे परिवार टूटने लगे हैं।
6. विवाह के रूप में परिवर्तन – विवाह की आयु में भी वृद्धि हो गई है। पहले बाल विवाहों का प्रचलन था। अब ‘शारदा एक्ट’ पारिक करके बाल विवाह के आदर्श को समाप्त कर दिया गया है। अब बड़ी आयु में विवाह होने लगे हैं तथा प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि का प्रचलन हो गया है।
7. विवाह के आदर्शों में परिवर्तन – परंपरागत रूप में हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता था किंतु आज विवाह एक समझौता बन गया है, जो कभी-कभी किन्हीं विशेष दशाओं में तोड़ा जा सकता है। साथ ही, आज हिंदू समाज में विवाह-विच्छेद की दर बढ़ती जा रही है।
8. विधवाओं की स्थिति में सुधार – विधवाओं को पुनर्विवाह करने की छूट मिल गई है। आज सभी को समानता के अधिकार प्राप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियाँ घर से बाहर जाकर नौकरियाँ कर सकती हैं।
(ख) दार्शनिक पहलुओं में परिवर्तन
सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत में दार्शनिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है –
1. समाज में शक्ति का संचार – वेदान्त दर्शन द्वारा शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के भ्रष्टाचार को दूर करके समाज को पुनः शक्तिशाली बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी भाँति, अन्य धर्मों की कुरीतियों की समाप्ति हेतु चलाए गए समाज-सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ है।
2. सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन – भारत में जब कभी दार्शनिक विचार अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचकर समाज को दूषित करने लगे तभी उनके विरुद्ध आंदोलन हुआ है। वैदिक कर्मकांडों के दोषों का विरोध करने के लिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का जन्म हुआ जिनसे व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है।
3. अध्यात्मवाद पर प्रभाव – भारतीय दर्शन एवं परंपरागत चिंतन पर गाँधीवाद, माक्र्सवाद तथा महर्षि अरविंद के अध्यात्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है।
4. भारतीय संस्कृति में नया मोड – अंग्रेजी शासनकाल में महर्षि दयानन्द, महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमंहस आदि महान् विभूतियों ने भारत के सोए हुए समाज को जगाकर भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दे दिया। इसी का यह परिणाम है कि आज़ भारतीय संस्कृति पूर्णतया भौतिकवादी संस्कृति नहीं है। इसकी मौलिक दार्शनिक एवं संस्थागत धारणाएँ किसी-न-किसी रूप में आज भी यथावत् बनी हुई हैं।
(ग) सामाजिक संगठन पर प्रभाव
सामाजिक संगठन की आधारशिला जाति व्यवस्था है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन करके सामाजिक संगठन को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है –
1. मशीनों पर कार्य करने के कारण छुआछूत, खान-पान आदि के प्रतिबंध शिथिल पड़ गए हैं तथा जातीय दूरी कम हो गई है।
2. उद्योग-धंधों के विकास के कारण आर्थिक आधार पर संगठन बने और इससे जातीय भेदभाव समाप्त होने लगा है।
3. पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित विद्यालयों में सभी जातियों के छात्र एक साथ बैठकर पढ़ने लगे, जिससे छुआछूत का भाव समाप्त हो गया है।
4. भारतीय सरकार ने बाल विवाह, विवाह एवं विवाह-विच्छेद अधिनियमों को पारित करके जाति | प्रथा में घोर परिवर्तन किए हैं।
5. उद्योग-धंधों का विकास हो जाने से जजमानी प्रथा का महत्त्व कम हो गया है।
6. यातायात के साधनों के विकास से जनसंपर्क में वृद्धि हुई और संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ इससे जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़ गए हैं।
7. जातीय पंचायतों का महत्त्व कम हो रहा है। भारत में लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण के कारण जातिवाद का महत्त्व भी कम हो रहा है।
8. सरकार ने सभी को एक समान मौलिक अधिकार प्रदान करके अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है।
उक्त बातों से पता चलता है कि भारत में सामाजिक संगठन के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की गति काफी तीव्र रही है।
(घ) सामाजिक वर्गों में परिवर्तन
आज भारत में औद्योगीकरण हो जाने से सामाजिक वर्गों का आधार ही बदल गया है। आज समाज में आर्थिक आधार पर सामाजिक वर्गों का निर्माण हो रहा है। पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग आदि ऐसे वर्गों के कुछ उदाहरण हैं। वर्ग निर्माण के साथ ही संघवाद की भावना भी भारतीय समाज में विकसित हो गई है तथा आज प्रत्येक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक सचेत होते जा रहे हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय समाज में स्तरीकरण का रुख जाति से वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित होता जा रहा है।

(ङ) औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन
भारत में कल-कारखानों का विकास हुआ है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं प्राचीन उद्योग-धंधों (गुड़ बनाना, चरखा चलाना, कपड़ा बुनना आदि) में परिवर्तन हो गया है। अभी तक भारत में केवल कृषि ही मुख्य उद्यम था, किंतु आज भारत में उद्योग-धंधों का विकास हो जाने से आजीविका के अनेक साधन हो गए हैं। आज भारत विश्व के दस बड़े औद्योगिक देशों में से एक है। औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन ने भारतीय समाज के सभी पक्षों में परिवर्तन की गति को अत्यंत तीव्र कर दिया है। उदाहरणार्थ-मशीनों का प्रयोग हो जाने से बेकारी बढ़नी शुरू हो गई है, पूँजीपतियों तथा । श्रमिकों को संघर्ष आरंभ हो गया है तथा सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई है।
औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय सामाजिक संगठन में भी अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इससे भारतीय समाज के तीनों प्रमुखों स्तंभों ग्रामीण समाज, जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण जीवन आज रूढ़िवादी नहीं रह गया है तथा इस पर नगरीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जातीय दूरी निश्चित रूप से कम हुई है तथा ग्रामीण समाज में भी जाति एवं व्यवसाय का परंपरागत संबंध टूटता जा रहा है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं तथा संयुक्त परिवार की परपंरागत संरचना एवं कार्यों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को अनेक प्रक्रियाएँ (प्रथम सात कारण वस्तुतः परिवर्तन की प्रक्रियाएँ हैं) प्रोत्साहन दे रही हैं। इसकी गति एवं व्यापकता प्रत्येक्ष क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। लगभग सभी क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं से काफी प्रभावित हुए हैं।
प्रश्न 7.
अपराध, संघर्ष तथा हिंसा में संबंध विस्तार से स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
संघर्ष (विवाद), अपराध एवं हिंसा में घनिष्ट संबंध पाया जाता है। इन तीनों में संबंध को जानने से पूर्व इनका अर्थ समझना अनिवार्य है।
संघर्ष का अर्थ तथा परिभाषाएँ
संघर्ष एक चेतन एवं असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के हितों को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तथा बलपूर्वक एक-दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। संघर्ष को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है –
1. फिचर (Fichter) के अनुसार – “संघर्ष पारस्परिक अंत:क्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक-दूसरे को दूर रखने का प्रयास करते हैं।”
2. फेयरचाइल्ड (Fairchild) के अनुसार – “संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।
3. गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार – “संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है। | जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति विरोधी की हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा करते हैं।’
4. ग्रीन (Green) के अनुसार – “संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा पर जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे बलपूर्वक रोकने के प्रयास को कहते हैं।”
5. पार्क एवं बर्गेस (Park and Burgess)के अनुसार – “संघर्ष और प्रतियोगिता विरोध के दो रूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा सतत एवं अवैयक्तिक होती है जबकि संघर्ष का रूप असतत व वैयक्तिक होता है।”
6. कोजर (Coser)के अनुसार – ‘स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है जिनमें विरोधी दलों का उद्देश्य
अपने प्रतिस्पर्धा को प्रभावहीन करना, हानि पहुँचाना अथवा समाप्त करना भी है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा का प्रयोग करके या हिंसा का भय देकर करते हैं। यह प्रत्यक्ष और चेतन प्रक्रिया है जिसमें सामान्यत: दूसरे पक्ष को किसी-न-किसी प्रकार की हानि पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।
अपराध का अर्थ तथा परिभाषाएँ
कानून की दृष्टि से वह प्रत्येक कार्य करना अपराध है, जो कानून द्वारा वर्जित किया गया है। सामाजिक दृष्टि से अपराध सामाजिक नियमों एवं आदर्शों के विरुद्ध कार्य करना है। इसकी प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –
1. सदरलैंड एवं जैसे (Sutherland and Cressy)के अनुसार – “अपराधी व्यवहार वह व्यवहार | है जिससे अपराधी कानून भंग करता है।”
2. मावरर (Mowrer) के अनुसार – “अपराध सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है।”
3. सेथना (Sethna) के अनुसार – “अपराध कोई ऐसा कार्य या दोष है, जो कि देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है।”
4. हाल्सबरी (Halsbury)के अनुसार – “अपराध एक ऐसा कार्य या दोष है जो जनता के विरुद्ध | असंतोष है और जो कार्य के कर्ता या दोषी को दंड का भागी बनाता है।’
5. इलियट एवं मैरिल (Eliott and Merrill) के अनुसार – (अपराध की परिभाषा उस कानुन विरोधी व्यवहार के रूप में की जा सकती है, जिसको समूह ने न माना हो और जिसके साथ
समाज ने दंड की व्यवस्था की हो।’
6. टैफ्ट (Taft) के अनुसार – “अपराध वे कार्य हैं, जिनका करना कानून द्वारा रोका गया है और जो विधि द्वारा दंडनीय माने गए हैं।”
7. लैडिंस एवं लैडिंस (Landis and Landis) के अनुसार – “अपराध वह कार्य है, जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिप्रद घोषित किया है और जिसे दंड देने के लिए राज्य शक्ति
रखता है।”
इस प्रकार अपराध एक कानूनी एवं सामाजिक संकल्पना है। कानून की दृष्टि में राज्य के नियम या कानूनों का उल्लंघन करना ही अपराध है। कानून द्वारा ही यह निर्णय होता है कि कौन-सा कार्य अपराध है और कौन-सा नहीं, जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन कार्यों को अपराध माना जाता है जो सामाजिक नियमों, आदर्शों व आचरणों के विरुद्ध होते हैं। अन्य शब्दों में सामाजिक आदर्शों को आघात पहुँचाना ही अपराध है और आघात पहुँचाने वाला व्यक्ति अपराधी है। समाजशास्त्रियों के मत से, किसी विशेष समय में संस्थागत रीति-रिवाजों या मान्य लोकमत के विरुद्ध कार्य करने को अपराध कहा जाता है। मैनहिम (Mannheim) के अनुसार, अपराध का कानून से संबंध नहीं है। कानून के न होते हुए भी कुछ समाज-विरोधी कार्य अपराध कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार, समाज-विरोधी आचरण भी अपराध की कोटि में आते हैं। उन्हीं के शब्दों में, “अपराध कानून से संबंधित नहीं होते हैं।……..कानून के अभाव में भी कुछ समाज-विरोधी कार्य अपराध की कोटि में रखे जाते हैं और मानवीय आचरण का कोई भी रूप, जो समाज के आदर्शों के विरुद्ध नहीं है, अपराध नहीं माना जा सकता है। क्लीनार्ड (Clinard) के अनुसार, “अपराध सामाजिक आदर्शो से विचलन है।”

हिंसा का अर्थ तथा परिभाषाएँ
अनेक व्यक्ति एवं समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। हिंसा का अर्थ खून-खराबे से है। विध्वंस, विनाश एवं क्षति के कार्यों को हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। मारपीट, अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं का विक्रय, चोरी, डाका, अंग-भंग करना, हत्या करना, घर जला देना, धोखा देना, दंगा करना, लूटमार करना, व्यक्तिगत व सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, आँसू गैस व लाठी चार्ज, देखते ही गोली मार देना, झूठी मुठभेड़ करके किसी को मार गिराना, पुलिस हिरासत में यातना देना व निर्दोष लोगों को हिरासत में ले लेना, आतंकवाद, विद्रोह, शीतयुद्ध, सैनिकों द्वारा आकस्मिक शासन परिवर्तन आदि हिंसा के ही विभिन्न रूप हैं।
हिंसा को मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को संक्रमणकालीन पहलू माना जाता है क्योंकि विकास के साथ-साथ हिंसा भी कम होती जाती है। परंतु यह एक सहज प्राकल्पना है जिसका आनुभविक आँकड़ों के आधार पर सत्यापन करना कठिन है। हिंसा के कार्य असंवैधानिक अथवा व्याधिकीय होते हैं। कई बार राज्य भी नागरिकों से कानून का पालन कराने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है। हिंसा के कार्य नैतिक दृष्टि से अच्छे, बुरे अथवा उदासीन हो सकते हैं तथा यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन कार्यों को कौन किसके विरुद्ध करता है तथा इसके प्रयोग का निर्णय लेने वाला कौन है। सी० राइट मिल्स (C. Wright Mills) के शब्दों में, शक्ति का अंतिम प्रकार हिंसा है।”
अपराध, संघर्ष तथा हिंसा में संबंध
संघर्ष को अपराध एवं हिंसा का कारण माना जाता है। सुविधासंपन्न समूह सुविधावंचित समूहों से भेदभावमूलक स्थिति बरतते हैं। इस स्थिति में ज्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। इसी भाँति, सुविधावंचित समूह सुविधासंपन्न समूहों से अपनी माँगों को लेकर संघर्ष करते हैं तथा माँगे न माने जाने पर हिंसा का भी प्रयोग करते हैं हिंसा अपराध में अंतर्निहित तत्त्व है क्योंकि अधिकांश अपराधों में हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ‘हिंसात्मक अपराध’ शब्द की उत्पत्ति इसी कारण हुई है। नैतिकता का ह्वास, राजनीति का अपराधीकरण तथा सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को संघर्ष, अपराध एवं हिंसा के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
प्रश्न 8.
प्रभाव, सत्ता एवं कानून की संकल्पनाएँ स्पष्ट कीजिए। इनमें क्या संबंध पाया जाता है? समझाइए।
या
शक्ति एवं सत्ता में अंतर बताइए।
या
कानून तथा सत्ता में क्या संबंध पाया जाता है? सत्ता का क्या अर्थ है? सत्ता के अर्थ की विवेचना कीजिए।
उत्तर
प्रभाव का अर्थ
व्यक्ति समाज में अकेले नहीं रहते अपितु अन्य व्यक्तियों के साथ रहते हैं। व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के जाल से ही समाज का निर्माण होता है। एक साथ रहने के कारण उनके संबंधों में एक-दूसरे का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति अन्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। लैसवेल एवं कांपलान (Lasswal and Kaplan) के अनुसार प्रभाव से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों की नीतियों को प्रभावित करना है। यह किसी व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छानुसार दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों को परिवर्तित करने की क्षमता है। इसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे अन्यथा वे नहीं कर पाते। प्रभाव में दो तत्त्व प्रमुख माने जाते हैं-अंत:संबंध तथा आशय। प्रभाव में ‘अंत:संबंध’ पाए जाते हैं। अर्थात् प्रभाव स्वयं अपने पर न होकर अन्य व्यक्तियों पर होता है। इसका दूसरा तत्त्व प्रभावित करने वाले व्यक्ति का आशय है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य से उसका आशय न होते हुए भी। स्वतः प्रभावित हो जाता है तो उसे प्रभाव नहीं कहा जाएगा। किस पर किसका कितना प्रभाव है, इसे मापना कठिन है। शक्ति, सम्मान, ईमानदारी, स्नेह, कुशल-क्षेम, धन-दौलत, प्रबोधन एवं कुशलता को प्रभाव से संबंधित मूल्य बताया गया है। प्रथम चार को सम्मान-मूल्य तथा अंतिम चार को कल्याण-मूल्य कहते हैं।
सत्ता का अर्थ
राजनीतिक शक्ति समाज में स्थायित्व बनाए रखने, उसका संचालन करने तथा समाज में निरंतरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक शक्ति में बल प्रयोग किया जाता है अथवा प्रयोग करने की धमकी दी जाती है जिससे व्यक्तियों को अनुपालन करने के लिए बाध्य किया जाता है तथा इसी से समाज में स्थायित्व आता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समाज में स्थायित्व इसलिए नहीं आता कि राजनीतिक शक्ति में बल प्रयोग किया जाता है अपितु इसलिए आता है कि शक्ति को वैधता मजबूत करती है। जब राजनीतिक शक्ति के साथ वैधता को जोड़ दिया जाता है तो उसे सत्ता कहते हैं। वेबर के अनुसार सत्ता का संबंध शक्ति से है। वैध शक्ति (Legitimate power) को ही सत्ता कहा जाता है। सत्ता द्वारा ही सामाजिक क्रिया का परिसंचालन होता है तथा इसी के द्वारा समाज में स्थायित्व बना रहता है अथवा सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होता है।
वेबर की सत्ता संबंधों की चर्चा अर्थात् कुछ व्यक्तियों के पास शक्ति कहाँ से आती है तथा वे यह अनुमान क्यों लगाते हैं कि अन्य व्यक्तियों को उनको अनुपालन करना चाहिए, वास्तव में, उनके आदर्श प्रारूप का ही एक उदाहरण है जिसमें वह सत्ता को तीन श्रेणियों में वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। सत्ता केवल राजनीतिक क्रियाओं अथवा परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं है अपितु सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्ता क्रियाशील है तथा देखी जा सकती है। राजनीतिक तथा सामाजिक पहलुओं में अंतर केवल इतना है कि पहले में सत्ता इसके साथ जुड़ी हुई है, जबकि दूसरे में शक्ति तथा सत्ता का वितरण समान रूप से नहीं है।
सत्ता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है –
ब्रीच (Beach)के अनुसार – “दूसरों के कार्यों अथवा कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहा जाता है।”
मैकाइवर (Maclver) के अनुसार – “सत्ता को प्रायः शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।’
दहल (Dahl)के अनुसार – “औचित्यपूर्ण शक्ति या प्रभाव को प्रायः सत्ता कहा जाता है।”
बीरस्टीड (Bierstedt) के अनुसार – “सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्ःत्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है।”
सत्ता को अधीनस्थों द्वारा इस कारण स्वीकार किया जाता है कि यह उनकी सहमति पर आधारित होती है। अधीनस्थ ही यह स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत उचित है अथवा नहीं। अतएव सत्ता को इस कारण स्वीकार नहीं किया जाता है कि वह अधिकारियों द्वारा लागू की जाती है। आदेश देने वाले अधिकारी को अधिकारी उसी अवस्था में कहा जाता है जबकि उसके द्वारा दिए गए आदेशों का स्रोत सही व उचित हो। यह भी कहा जा सकता है कि सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति का प्रयोग है। सत्ता उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने समान बनाकर प्रभावित करने का साधन है।
कानून का अर्थ
साधारण व्यक्ति के मन में ‘कानून’ शब्द का आशय नियमों के व्यवस्थित संग्रह से है, परंतु यह सामान्य अर्थ कानून की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाता। वस्तुत: कानून आचरण के वे नियम हैं। जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। इन्हें व्यक्तियों के आचरणों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने हेतु राज्य द्वारा सोच-विचारकर निर्मित किया जाता है।
‘कानून जर्मन भाषा के शब्द ‘लैग’ (lag) का हिंदी रूपांतर है। इसको शब्दिक अर्थ है-‘जो सर्वत्र एक-सा रहे। अंग्रेजी भाषा में भी इसी शब्द का यही अभिप्राय है। कानून का यही अर्थ वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय नियमों पर भी लागू होता है। अतः आधुनिक काल में समाज को सुव्यवस्थित, स्थिर एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए राज्य अथवा सरकार द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है वे नियम ही कानून कहलाते हैं। प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है
कारडोजो (Cardozo) के अनुसार – “कानून आचरण का वह सारभूत नियम है जिसे हम निश्चितता से प्रपिादित किया जाता है कि यदि भविष्य में उसकी सत्ता को चुनौती दी गई तो उसे अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा।’
मजूमदार एवं मदन (Majumdar and Madan) के अनुसार – “कानून सिद्धांतों का वह समूह है जो कि भू-भाग में राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन को स्थापित रखने के लिए शक्ति के प्रयोग की आज्ञा । देता है।”
मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार – “कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए स्वीकृत, प्रतिपादित एवं लागू किए जाते हैं।”
ग्रीन (Green) के अनुसार – “कानून परिवर्तन के तथ्य एवं निष्पादन की कल्पना के मध्य संतुलित सामान्यीकृत नियमों का न्यूनाधिक क्रमबद्ध समूह है जो विशिष्ट रूप से परिभाषित संबंधों एवं स्थितियों को शासित करता है तथा परिभाषित एवं सीमित ढंग से बल अथवा उसके भय को प्रयुक्त करता है।”
समाजशास्त्रीय साहित्य में कानून की व्याख्या निम्नलिखित चार अर्थों में की गई है –
1. सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में कानून – कानून को सामाजिक निंयत्रण के रूप में देखने संबंधी विचारधारा का सूत्रपात में मैलिनोव्स्की (Malinowski) ने किया था। यद्यपि उनके मूल विचारों में आज बहुत संशोधन हो गया है तो भी उनके अंश महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। आजकल रॉसको पाउंड (Roscoe Pound) की कानून की परिभाषा अधिक स्वीकृत की जा रही है जिन्होंने कानून को एक ऐसा सामाजिक नियंत्रण माना है जो राजनीतिक रूप से संगठित “समाज की शक्ति द्वारा संचालित होता है।
2. प्रक्रिया के रूप में कानून – कुछ विद्वानों ने ‘कानून’ शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया है जो कानून के निर्माण, कानून को लागू करने एवं कानून के निर्वचन एवं निर्णयन से संबंधित है। इस अर्थ में कानून संबंधी तीनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जिसमें कानून बनाना, लागू करना एवं मुकदमों का फैसला करना शामिल है।
3. व्यापक अवधारणा के रूप में कानून – इस अर्थ में कानून से आशय आचरण के उन सभी प्रतिमानों (Norms) से लगाया जाता है जो किसी निश्चित काल-बिंदु पर समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनके उल्लंघन पर समाज कड़ी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है। इस अर्थ में कानून का प्रयोग दुर्वीम, हॉब्स तथा लॉक ने किया है। इस दृष्टि से ‘कानून’ शब्द में दोनों ही प्रकार के व्यवहार-नियम आ जाते हैं—प्रथागत नियम एवं अधिनियम के रूप में पारित कानून।
4. संकुचित अवधारणा के रूप में कानून – इस अर्थ में कानून उन सभी अधिनियमों को कहते हैं जो किसी समाज में सर्वोच्च सत्ता द्वारा सोच-विचारकर बौद्धिक रूप में पारित किए जाते हैं। इस अर्थ में औपचारिक रूप से पारित अधिनियम ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रायः विधिशास्त्रियों द्वारा इसी अर्थ में ‘कानून’ शब्द का प्रयोग किया जाता है।
प्रभाव, सत्ता एवं कानून में संबंध
प्रभाव, सत्ता एवं कानून की संकल्पनाएँ परस्पर जुड़ी हैं। जब शक्ति के साथ बाध्यता समाप्त हो जाती है तथा लोग स्वयं उस शक्ति को स्वीकार करने लगते हैं तो उसे प्रभाव कहा जाता है। यदि शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो उसे सत्ता कहा जाता है। आधुनिक समाजों में शक्ति को वैधता प्रदान करने में कानून की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभाव शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है पंरतु अधिकांशतः शक्ति कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है जिसका एक वृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। प्रभाव, कानूनी सत्ता तथा कानून सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
शक्ति एवं सत्ता में अंतर
शक्ति एवं सत्ता ‘शक्ति शब्दावली’ की दो प्रमुख अवधारणाएँ हैं। वैध अनुमोदन या संस्थागत शक्ति को ही सत्ता कहा जाता है। दोनों में पायी जाने वाली प्रमुख असमानताएँ निम्नांकित हैं –
- समाज में सत्ता शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है।
- सत्ता की अपेक्षा शक्ति एक अधिक व्यापक अवधारणा है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि सत्ता शक्ति का एक विशेष प्रकार है।
- शक्ति वैध तथा अवैध दोनों प्रकार की होती है, जबकि सत्ता केवल वैध शक्ति को ही कहा जाता है।
- शक्ति दंडभय द्वारा व्यक्तियों से अनुपालन करवाने की क्षमता है, जबकि सत्ता का अनुपालन ऐच्छिक कार्य होता है।
- समाज के स्थायित्व एवं निरंतरता में सत्ता का योगदान शक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- क्योंकि सत्ता वैध शक्ति है इसलिए इसके साथ वैधता सदैव जुड़ी रहती है। अन्य शब्दों में, शक्ति को वैधता प्रदान करके सत्ता में परिवर्तित किया जा सकता है।
अत: हम यह कह सकते हैं कि सत्ता शक्ति का वैध रूप है। यदि कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डाँटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और सत्ता कहा जाएगा, क्योंकि बच्चों को समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाना; पिता, माता व परिवार का मुख्य कार्य है। यदि कोई बदमाश मुहल्ले वालों को किसी कार्य के लिए तंग करता है तो उसे शक्ति कहा जाएगा क्योंकि बदमाश के पास मुहल्ले वालों से उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रश्न 9.
नगर एवं कस्बे की अवधारणाएँ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
कस्बा, नगर एवं नगरीकरण तीन परस्पर संबंधित अवधारणाएँ हैं। कस्बा गाँव एवं नगर के बीच की श्रेणी है। कई बार कस्बे को ‘उप-नगर’ भी कहा जाता है। नगरीकरण किसी भी देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित प्रकिया है। इन तीनों अवधारणाओं में नगरीकरण का अर्थ तो स्पष्ट है परंतु ‘कस्बा’ एवं ‘नगर’ शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न रूपों में किया जाता है।
नगर की अवधारणा
‘नगरीय समुदाय’, ‘नगरीय क्षेत्र तथा ‘नगर’ (शहर) पर्यायवाची शब्द है जिनकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न देशों में नगरीय शब्द का अर्थ एक जैसा नहीं है। भारत में नगरीय क्षेत्र का संबंध कस्बों तथा नगरों दोनों से है। इसीलिए भारत में नगर को कस्बे से भिन्न बताने के लिए कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यत: गैर-कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं। अत: ‘नगरीय’ शब्द का प्रयोग कस्बे, नगर, उप-नगर, महानगर, विश्व-नगर इत्यादि शब्दों के स्थान पर किया जाता है। नगर से अभिप्राय एक ऐसे केंद्रीयकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। 1991 ई० की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 4,689 नगर थे जिनमें महानगर एवं विराट नगर भी सम्मिलित थे।
नगर की परिभाषा देना भी एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। किंग्स्ले डेविस (Kingsley Davis) इससे बिलकुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की उपज होती है। उनके अनुसार नगर ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है। यह कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। सोमबंर्ट (Sombart) ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए इस संदर्भ में कहा है-“नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं।’ लुईस विर्थ (Louis Wirth) ने द्वितीयक संबंधों, भूमिकाओं के खंडीकरण तथा लोगों में गतिशीलता की तेजी इत्यादि विशेषताओं के आधार पर नगर को परिभाषित करने पर बले दिया है।
विर्थ के अनुसार अपेक्षाकृत एक व्यापक, घना तथा सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों
का स्थायी निवास क्षेत्र है। इन्हीं के आधार पर नगरीय समुदाय के लक्षण निश्चित किए जाने चाहिए। ‘नगर’ के साथ-साथ ‘महानगर’ (Metropolis), ‘विराट नगर’ (Mega City or Megalopolis), ‘विश्व-नगर’ (Cosmopolis or Cosmopolitan City or Ecumenopolis) तथा नगर-समूह (Conurbation) इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब शब्दों में जनंसख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्वं, आवागमन एवं संचार साधनों की सुविधाओं इत्यादि के आधार पर अंतर किया जाता है।
भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को ‘विराट नगर’ कहा जाता है। 1991 ई० की जनगणना के अनुसार केवल 4 विराट नगर थे—मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ‘विश्व-नगर’ हेतु जनसंख्या के आकार को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है। विश्व-नगर उसे कहा जाता है जहाँ विश्व के अधिकांश भागों के लोग रहते हों। भारत में पांडिचेरी को विश्व-नगर माना जाता है। वैसे चारों विराट नगर भी एक प्रकार से विश्व-नगर ही हैं। ‘नगर-समूह’ अथवा ‘कोनबेशन’ शब्द से अभिप्राय निरंतर विस्तारित होते हुए ऐसे नगरीय क्षेत्र से है जिसका रचना कई पूर्व पृथक् नगरों द्वारा हुई होती है। दिल्ली कोनर्देशन तथा कोलकाता कोनर्देशन ‘नगर-समूह’ के उदाहरण हैं।
कस्बे की अवधारणा
जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गाँवों के लोगों की प्रवृत्तियाँ नगरीकृत हो जाती है तो उन्हें गाँव न कहकर ‘कस्बा’ कहा जाता है। इस प्रकार, कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने
जीवनक्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों प्रकार के तत्वों को अंतर्निहित करता है। | बर्गल (Bergal) के शब्दों में, “कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता
है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। किसी पिछड़े हुए अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जब किसी नगर के साथ संपर्क स्थापित होता है तो उनमें धीरे-धीरे नगरीय लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी से गाँव का रूप एक कस्बे के रूप में बदल जाता है परंतु त – ध्यान देने योग्य है कि क़स्बे को केवल बड़े गाँव के रूप में ही परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि गाँव और कस्बे में काफी अंतर होता है। गाँव की तुलना में कस्बा बहुउद्देश्यीय होता है। कस्बों में बैंक, बीमा कंपनियों के दफ्तर, आवागमन के साधन और स्वास्थ्य सुविधाएँ गाँव की तुलना में अधिक होती है। कस्बा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी संपादित करता है।
किसी पिछड़े या ग्रामीण क्षेत्र पर जब मानवीय जनसंख्या स्थायी रूप से निवास करने लगती है और उस जनसंख्या का उद्देश्य धर्म, कला, साहित्य, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा आदि का प्रसार होता है तो उसे हम ‘कस्बा’ कहते हैं। मेयर एवं कोहन (Mayer and Kohn) ने कस्बे को मानवीय प्रक्रिया का परिणाम माना है क्योंकि इसका विकास गाँव की संपन्नता एवं उसमें नगरीय लक्षणों के आ जाने से होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कस्बा बड़ा गाँव नहीं है। कस्बा अपनी संपूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है, जबकि गाँव के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाहरी जगत पर ही आश्रित होते हैं। कस्बे पर अनेक पड़ोसी गाँव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आश्रित होते हैं। यह इन गाँववासियों के लिए एक प्रकार से नगर का कार्य करता है।
भारत में कस्बे की परिभाषा विभिन्न जनगणना वर्षों में बदलती रही है। उदाहरणार्थ-1901 ई० की जनगणना में कस्बा उस निवास क्षेत्र को कहा गया जिसमें निम्नलिखित चार विशेषताएँ थीं–
- किसी भी आकार की नगरपालिका,
- सिविल लाइन का क्षेत्र जो नगरपालिका के अंतर्गत न हो.
- प्रत्येक प्रकार का छावनी क्षेत्र तथा
- वह स्थायी निवास स्थान जहाँ कम-से-कम 5,000 की जनसंख्या हो।
1921 ई० की जनगणना में कस्बा उस नगरीय लक्षणों वाली बस्ती को कहा गया है जहाँ 5,000 से अधिक लोग स्थायी रूप से निवास करते हों। तत्पश्चात् 1961 ई० एवं उसके पश्चात् होने वाली जनगणनाओं में कस्बे की अधिक विस्तृत परिभाषा दी गई। अब कस्बे के निर्धारण में निम्नलिखित कसौटियों को अपनाया जाता है।
(अ) वे सभी स्थान जहाँ नगर महापालिका, कैंट बोर्ड अथवा अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति इत्यादि हैं; तथा
(ब) वे सभी स्थान, जहाँ
- कम-से-कम 5,000 की आबादी है,
- कार्यरत पुरुष जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग गैर-कृषि व्यवसाय में लगे हुआ है तथा
- प्रति वर्गमील 400 व्यक्तियों का घनत्व है।
प्रश्न 10.
गाँव किसे कहते हैं? भारतीय गाँव की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
या
गाँव को परिभाषित कीजिए तथा गाँवों के प्रमुख प्रकार बताइए।
या
भारत के संदर्भ में गाँवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? समझाइए।
उत्तर
गाँव, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है, जो कि समाजशास्त्र की प्रमुख शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय-वस्तु और क्षेत्र; ग्रामीण जीवन और समुदाय से संबंधित हैं। इस दृष्टि से भारतीय गाँव का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। प्रायः सभी भारतीय गाँवों में किसी-न-किसी मात्रा में समानता पायी जाती है। भारत में आदिकाल से गाँव पाए जाते रहे हैं और इन गाँवों में अपने युग की छाप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में अनेक विदेशी शासक आए और उन्होंने भारत पर शासन किया। इन विदेशी शासकों का भारतीय ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव अवश्य पड़ा, किंतु उनमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। भारत में गाँव विविधता में एकता के द्योतक माने जाते हैं। इस दृष्टि से गाँवों का अध्ययन आवश्यक है।
गाँव का अर्थ तथा परिभाषाएँ।
गाँव वैसे तो एक अत्यंत सरल शब्द लगता है परंतु इसकी कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। इसे परिवारों का वह समूह कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित होता है तथा जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। गाँव की एक निश्चिम सीमा होती है तथा गाँववासी इस सीमा के प्रति सचेत होते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से पता होता है कि उनके गाँव की सीमा ही उसे दूसरे गाँवों से पृथक् करती है। इस सीमा में उस गाँव के व्यक्ति निवास करते हैं, कृषि तथा इससे संबंधित व्यवसाय करते हैं तथा अन्य कार्यों का संपादन करते हैं। भारतीय गाँवों के घरों की दीवारें अधिकांशतः मिट्टी की होती हैं। उनकी छत खपरैल की होती हैं। आवागमन के लिए कच्ची गलियाँ होती हैं। भारतीय गाँव अपेक्षाकृत एक परिपूर्ण इकाई होते थे, यद्यपि अब इनमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील है। इनमें जजमानी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। धर्म और परंपराओं का ग्रामीण जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।
विभिन्न विद्वानों ने गाँव की जो परिभाषाएँ की हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं –
1. आर० के० पाटिल (R.K. Patil) के अनुसार – “ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य ग्राम स्थान पर समीपस्थ गृहों में निवास करने वाले परिवारों के समूह को सामान्यतः ग्राम की अभिव्यक्ति के • रूप में समझा जा सकता है।”
2. ए० आर० देसाई (A.R. Desai) के अनुसार – “गाँव ग्राम्य समाज की इकाई है। यह रंगशाला के समान है, जहाँ ग्राम जीवन को प्रकट करता है और कार्य करता है।”
3. सिम्स (Sims) के अनुसार – “गाँव वह नाम है, जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को । साधारणतयाः दर्शाता है।”
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाँव मानव निवास का वह नाम है, जिसका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है और जहाँ सामुदायिक जीवन के सभी तत्त्व पाए जाते हैं। यहाँ निवास करने वाले सदस्य पारस्परिक आत्म-निर्भरता के द्वारा सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं।
गाँव की ऐतिहासिक रूपरेखा
गाँव की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि गाँव की उत्पत्ति का प्रमुख आधार सभ्यता का विकास है। सभ्यता के विकास ने मनुष्य के ज्ञान को विकसित किया जिसके फलस्वरूप विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने विभिन्न प्रयत्न प्रारंभ किए और विभिन्न अनुभवों एवं प्रयत्नों के उपरांत संतोष प्राप्त किया। यह प्रक्रिया कालांतर में निरंतर रही है और वर्तमान समय में गाँव संरचना से कस्बों, नगरों और शहरों की संरचना विकसित हुई है। अनेक उविकासवादियों का यह मत है कि कृषि के उदय के बाद गाँव का संगठन दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार गाँव के विकास के बारे में एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि गाँव के विकास के कारक इतने समीपवर्ती और अस्पष्ट हैं कि इनसे कोई स्थायी कल्पना निर्धारित नहीं की जा सकती। गाँव निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में रहता हैं। ये परिवर्तन प्रौद्योगिक-आर्थिक, सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक आदि शक्तियों के कारण प्रभावित होते रहे हैं।
इस समस्या के निवारण हेतु भी विभिन्न विचारकों ने अपने मत प्रकट किए हैं। ए० आर० देसाई (A.R. Desai) ने कहा है-“पर्यावरणीय एवं क्षेत्रीय प्रयत्न ग्राम्य प्रारूपों एवं ग्राम्य सामाजिक संरचना में विभेद करने में सहायता करेंगे। ये प्रयत्न प्रादेशीय, जिले संबंधी एवं क्षेत्रीय इकाइयों के वैज्ञानिक वर्गीकरण में भी सहायक होंगे। ये विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रों के निर्माण के आधारभूत तत्त्वों की स्थापना में भी सहायक होंगे और अंत में ये संपूर्ण रूप में भारतीय समाज के व्यवस्थित वर्णन को विकसित करने में सहायक होंगे। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रयास गाँव के विकास को निर्धारित करने के लिए किए। और इसी कारण गाँव के विकास के संबंध में विभिन्न विचार पारित हुए। देसाई ने लिखा है-“गाँव का उदय इतिहास में कृषि अर्थव्यवस्था के उदय के साथ संबंद्ध है। गाँव का उदय यह निर्देशित करता है कि मानव सामूहिक घुमक्कड़ जीवन से गुजरकर स्थायी जीवन में आया है। यह मूलरूप से उत्पादन के यंत्रों के सुधार के परिणामस्वरूप हुआ, जिसने कृषि का विकास किया और इस भाँति एक निश्चित सीमित क्षेत्र में स्थायी जीवन को संभव और आवश्यक बनाया। जो व्यक्ति स्थायी कृषि को ही ग्रामोदय का आधार मानते हैं उनको विश्वास है कि गाँवों का उदय सभ्यता के उदय के साथ-साथ स्थायी कृषि के परिणामस्वरूप हुआ है।
स्थायी कृषि के कारण गाँव सामूहिक स्थापना का प्रथम रूप है। और ग्रामीण कृषि इस व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रथम कारक है। कृषि में उत्पादन बढ़ने के अतिरिक्त खाद्य सामग्री के बच जाने से व्यक्ति अन्य उद्योगों की ओर बढ़े और कस्बों व नगरों की स्थापना हुई। कुछ विद्वान कृषि के अतिरिक्त गाँवों का उदय मानवीय जीवन के उदय के साथ भी निर्धारित करते हैं। पंरतु उविकासवादी कृषि के कारक पर ही अधिक बल देते हैं। वास्तव में जब मानव की सामूहिक व घुमक्कड़ प्रवृत्ति को यांत्रिक व स्थायी खेती का साधन प्राप्त हुआ तो उसी समय से निवास व्यवस्था ने भी स्थायी रूप धारण किया। इसी के फलस्वरूप गाँवों का निर्माण व विकास प्रारंभ हुआ। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शिकारी व घुमक्कड़ अर्थात् खाद्य संकलन की अवस्था को हो (लकड़ी को नुकीला कर कृषि हेतु प्रयोग करना) के आविष्कार ने स्थायी रूप में परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन के उपरांत पशुपालन का महत्त्व बढ़ गया तथा गाँव का संगठन विकसित हुआ। इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्री सिम्स (Sims) ने भी लिखा है-“गाँव प्राचीन कृषकों की स्थापना को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यत: प्रयोग किया जाने वाला नाम है।” भूगोलशास्त्रियों का यह मत है कि कृषि ने मानवीय जीवन में सुरक्षा तथा स्थायित्व प्रदान किया है। कृषि के उपरांत ही सभ्यता का विकास एवं गाँव संरचना में वृद्धि हुई है।
गाँव के विकास के बारे में जे० बी० रोज (J.B. Rose) का कहना है–“प्रथम अवस्था अग्रगामी काल की अवस्था थी जो प्रारंभिक स्थापनाओं के काल से पूर्व लगभग 1800 ई० 1835 ई० तक तथा बाद में मध्य-पश्चिम के विभिन्न भागों में प्रसारित हुई। दूसरी अवस्था, जो भूमि जोतने का काल कहलाती है, ने अग्रगामी काल का उत्तराधिकार लिया और साधारणतः 1890 ई० तक रही। यह काल ग्रामीण समाज का विशिष्ट काल कहलाता है, क्योंकि इसी समय निवास स्थानों की सुव्यवस्था, स्कूल व धर्म-स्थानों का आयोजन हुआ था। तीसरी अवस्था विनाश अथवा विध्वंस काल कहलाती है जो 1890 ई० में मध्य-पश्चिम से प्रारंभ हुई और 1920 ई० तक समस्त देशों में फैल गई। यह काल भूमि वरदान और विशेषीकरण के काल के नाम से परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार जे०बी० रोज के विचारानुसार कृषि के पूर्व ही समाज स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और कृषि का कार्य बाद में अर्थात् दूसरी अवस्था में प्रारंभ हुआ था। विल्सन (Wilson), जिन्होंने कृषि के उदय के साथ ही गाँवों का उदय निर्धारित किया, के मत का विरोध करते हुए सिम्स (Sims) ने लिखा है।”
“ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति हमें पीछे सभ्यता के प्रांरभ की ओर, स्वयं स्थायी स्थापनों की ओर ले जाती है।” सभ्यता के उदय व स्थायित्व ने सामूहिक जीवन को कृषि के लिए बाध्य किया और तदुपरांत ही उपज का संकलन प्रारंभ हुआ। मानव अपनी क्षुधा तृप्ति हेतु ही इधर-उधर घूमता था। क्षुधा तृप्ति ही उसका तथा उसके जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य था। स्थायी जीवन के साथ ही उसे इस दिशा की ओर प्रयास करना अनिवार्य था। कृषि एक गाँव का एक सम्मिलित रूप इसीलिए ही आज हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी दृष्टि से प्राचीन गाँव कृषि व कृषक के नाम से ही संबंधित किए जाते हैं।
गाँवों के प्रमुख प्रकार
गाँवों के प्रमुख प्रकारों के बारें में भी विद्वानों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है। भारत के संदर्भ में विद्वानों ने गाँवों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है –
1. कोल्ब (Kolb) ने ग्रामीण जीवन में उपलब्ध सुविधाओं को ग्रामीण वर्गीकरण का आधार माना। है। इसी दृष्टि से उन्होंने गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है –
- सहज सुविधा वाले गाँव
- सीमित सुविधा वाले गाँव,
- अपर्याप्त सुविधा वाले गाँव,
- पूर्ण/आंशिक सुविधा वाले गाँव तथा
- पूर्ण नगरीय सुविधायुक्त गाँव।
2. एस० सी० दुबे (S. C. Dube) के अनुसार भारतीय गाँवों या ग्रामीण समुदाय के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया है –
- आकार, जनसंख्या और भू-भाग के आधार पर,
- प्रजातीय संगठन और जाति संरचना,
- भूस्वामित्व के प्रतिमान,
- अधिकार संरचना और शक्ति का सोपान क्रम,
- सामुदायिक अलगाव की मात्रा तथा
- स्थानीय परंपराएँ।
3. सोरोकिन (Sorokin) के अनुसार जिमरमैन और गाल्पिन ने भू-स्वामित्व को ग्रामीण वर्गीकरण का आधार माना है, जो निम्नलिखित हैं –
- संयुक्त भू-स्वामित्व वाले गाँव,
- पट्टीदारी व्यवस्था वाले गाँव,
- व्यक्तिगत भू-स्वामित्व वाले गाँव,
- वह गाँव जहाँ पट्टीदार रहते हैं,
- जहाँ जमींदारों के कारिंदे रहते हैं तथा
- जहाँ नौकरीपेशा लोग तथा श्रमिक निवास करते हैं।
4. ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से – ऐतिहासिक विकास-क्रम की दृष्टि से गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- कृषकों का सामूहिक स्वामित्व ग्राम,
- कृषकों के सामूहिक किराएदारी ग्राम,
- कृषकों का व्यक्तिगत स्वामित्व ग्राम,
- कृषकों के व्यक्तिगत किराएदारी ग्राम,
- व्यक्तिगत कृषक मजदूरों के ग्राम तथा
- राज्य व धर्म, कृषक मजदूरों के ग्राम।
5. संरचना के आधार पर – कर्वे (Karve) का विचार है कि संरचना ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार है। अतः इन्होंने गाँव की संरचना को ध्यान में रखकर गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है
- बिखरे हुए गाँव तथा
- समूह गाँव।
6. भूमि-व्यवस्था के आधार पर – बेडन पावेल (Baden Powell) ने भूमि व्यवस्था के आधार पर गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है –
- रैयतवारी गाँव तथा
- सामूहिक गाँव।
7. भारतीय गाँवों का सामान्य वर्गीकरण – जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से भारत एक विशाल देश है। इस विशालता के कारण भारतीय गाँवों का वर्गीकरण एक समस्या है। भारतीय गाँवों का वर्गीकरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है –
(i) जनसंख्या के आधार पर – जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- बड़े गाँव,
- मध्यम गाँव तथा
- छोटे गाँव।
बड़े गाँवों की श्रेणी में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को सम्मिलित किया जा सकता है। छोटे गाँवों के अंतर्गत 500 से कम आबादी वाले गाँवों को सम्मिलित किया जाता है। जो गाँव 500 से अधिक तथा 5,000 से कम की आबादी के हैं, उनहें मध्यम श्रेणी के गाँवों में सम्मिलित किया जा सकता है।
(ii) क्षेत्रफल के आधार पर – क्षेत्रफल के आधार पर गाँवों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- सीमित गाँव तथा
- विस्तृत गाँव।
विस्तृत गाँव वे हैं, जो विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। इनका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। इसके विपरीत सीमित क्षेत्रफल में फैले गाँव ‘सीमित गाँव’ के अंतर्गत रखे जा सकते हैं।
(iii) अर्थव्यवस्था के आधार पर – अर्थव्यवस्था के आधार पर गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- कृषिप्रधान गाँव,
- उद्योगप्रधान गाँव तथा
- मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गाँव।
कृषिप्रधान गाँव वे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। इन गाँवों में निवास करने वाले व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना है। इसके विपरीत उद्योगप्रधान गाँव वे हैं, जिनमें ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवन-यापन के लिए कुटीर उद्योग का संपादन किया जाता है। इन उद्योगों में लकड़ी, लोहा, मिट्टी, चमड़े आदि के उद्योग सम्मिलित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गाँव वे हैं, जहाँ कृषि तथा उद्योग दोनों का ही मिला-जुला स्वरूप पाया जाता है।
(iv) सुविधाओं के आधार पर – ग्रामीण जीवन में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- पूर्ण सुविधायुक्त गाँव,
- आंशिक सुविधायुक्त गाँव तथा
- सुविधाहीन गाँव।
पूर्ण सुविधायुक्त गाँवों की श्रेणी में उन गाँवों को रखा जाता है, जहाँ मानव जीवन की समस्त आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं में आवागमन तथा संचार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, व्यवसाय तथा व्यापार आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सुविधाहीन गाँव वे हैं, जहाँ उपर्युक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। आंशिक सुविधा युक्त गाँव इन दोनों के मध्य की स्थिति हैं, जहाँ कुछ सुविधाएँ भी हैं और कुछ असुविधाएँ भी।।
(v) परिस्थितिशास्त्रीय आधार पर – नगरीय और ग्रामीण परिस्थितियों के आधार पर गाँवों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- नगरीकृत गाँव,
- अर्द्ध-नगरीकृत गाँव तथा
- ग्रामीण गाँव।
नगरीकृत गाँवे वे हैं, जो विशाल नगरों के पास स्थित हैं। इन गाँवों की अर्थव्यवस्था तथा जीवन पूर्णतया नगरों पर आधारित होता है। इन गाँवों में कोलकाता, मुम्बई दिल्ली आदि के आस-पास स्थित गाँवों को सम्मिलित किया जा सकता है। ग्रामीण गाँव वे हैं, जो नगरीय सभ्यता से दूर स्थित हैं। वहाँ का वातावरण तथा जीवन ग्रामीण तत्त्वों पर आधारित है। अर्द्ध-नगरीय गाँव वे हैं, जो न तो पूर्णतया नगरीकृत हैं और न ही ग्रामीण।
(vi) अन्य वर्गीकरण – उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त गाँवों को अन्य अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित हैं
- धार्मिक आधार पर गाँवों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- धर्मप्रधान गाँव तथा
- मिश्रित धर्मप्रधान गाँव।
- शैक्षणिक आधार पर गाँवों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है –
- शिक्षित गाँव
- अर्द्ध-शिक्षित गाँव तथा
- अशिक्षित गाँव
- धार्मिक व राजनीतिक आधार पर गाँवों को सत्ता पक्ष और सत्ता विरोधी इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रश्न 11.
ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।
या
ग्रामीण समाज के परिवर्तित प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर
आज ग्रामीण समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से ग्रामीण जीवन काफी परिवर्तित होता जा रहा है। यह परिवर्तन इतना अधिक हुआ है कि ग्रामीण समाज को नगरीय समुदाय से भिन्न करना कठिन हो गया है।
ग्रामीण समाज के परिवर्तित प्रतिमान
भारतीय ग्रामीण सम्गज में होने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट देखा जा सकता है –
1. धार्मिक जीवन में परिवर्तन – बाह्य जगत का धार्मिक जीवन पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा है कि विस्तृत जगत के संपर्क में आकर गाँवों से धर्म और प्राचीन संस्कृति की रक्षा करने की भावनाओं का ह्रास होना प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण लोग आज बच्चों के जन्म के अवसर, कर्मकांडों, मृत्यु-भोज आदि पर पहले की अपेक्षा कम व्यय करने लगे हैं। धीरे-धीरे धार्मिक कृत्यों पर उनका विश्वास उठता चला जा रहा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण नैतिक मूल्यों को ह्रास होना प्रारंभ हो गया है। धर्म को ग्रामीण समाज में आजकल कम महत्त्व प्रदान किया जा रहा है। अधिकांश ग्रामीण लोग लौकिकीकरण (Secularization) से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।
2. राजनीतिक संरचना में परिवर्तन – स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण लोगों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति दिखाई है। ग्रामीण जनता ने राष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। अब ग्रामीण समुदाय केवल स्थानीय चुनावों तक ही सीमित नहीं रहता है, वरन् राज्य स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुनने में रुचि लेता है। अब वह विचारों की स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को समझ गया है। संचार के साधनों; जैसे—रेडियो, समाचार-पत्र इत्यादि ने ग्रामीण जगत के अंतर्गत राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। कुछ ग्रामीण लोग तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में ज्ञान भी रखते हैं। राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ ग्रामीण समाज में राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है, परंतु इतना सब-कुछ होते भी दुर्भाग्य की बात यह है कि गाँव आज दलबंदी के अखाड़े बन गए हैं, दलबंदी और दलबदलुओं को महत्त्व देने लगे हैं। फलस्वरूप कुछ ग्रामीण व्यवसायी राजनीतिज्ञ स्वयं तो राजनीति के शिकार होते ही हैं, साथ-ही-साथ अपने प्राचीन संगठन को भी खंडों में विभाजित कर बैठते हैं। वयस्क मताधिकार के कारण अब प्रभु-जातियों के परंपरागत प्रभुत्व को चुनौती दी जाने लगी है।
3. ग्रामीण आर्थिक संरचना में परिवर्तन – आज प्रत्येक किसान अपने परंपरागत कृषि-साधनों में परिवर्तन ले आया है। परंपरागत हल के स्थान पर ट्रैक्टर आ गए हैं। फलस्वरूप गाँवों में अन्न का उत्पादन बढ़ा है और अधिक आत्मनिर्भरता आ गई है। ग्रामीण समाज में अब वस्तुओं के विनिमय की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इसके साथ-ही-साथ जजमानी व्यवस्था भी समाप्त होती जा रही है। उसके स्थान पर पैसे से लेन-देन (Monetization) की भावनाएँ बढ़ रही हैं। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धंधे अब फैक्ट्रियों की ओर बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधी अधिनियमों ने कुछ परिवर्तन तो किया है, परंतु साथ-ही-साथ अधिकांश जनता में मुकदमों की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण समुदाय अब अधिक मुकदमेबाज हो गया है, अतः निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
4. संस्थागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन – इसके अंतर्गत हम शिक्षा, पारस्परिक संबंध, जाति, परिवार, जजमानी व्यवस्था, ग्रामीण गतिशीलता, आवास इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। पहले ग्रामीण लोग कम शिक्षित थे, परंतु अब शिक्षा की ओर उनकी रुचि बढ़ गई है और सब जाति और वर्ग के लोग कम-से-कम आगे आने वाली पीढ़ी को तो शिक्षा दिलाने के विचार से परिपूर्ण हैं। पारस्परिक संबंथों के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों में स्वार्थ की भावनाएँ बढ़ रही हैं तथा व्यक्तिवादी भावना का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जातिवाद की भावनाओं में भी लचीलापन आ गया है। स्वयं ग्रामीण लोगों की इस संबंध में यह धारणा बन गई है कि आजकल न तो कोई जाति है और न ही कोई धर्म। जजमानी व्यवस्था प्रायः अब टूट-सी गई है। परिजन लोग अब पैसा लेकर कार्य करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा आंशिक रूप में ही रह गई है। एकाकी परिवार बन रहे हैं। आवागमन के साधनों में प्रगति हो जाने से ग्रामीण गतिशीलता के स्तर में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से शिक्षित ग्रामीण तो अब नगर में ही अपनी जीविका कमाने में प्रतिष्ठा की बात समझता है और व्यवसाय के चल जाने पर या नौकरी मिल . जाने पर वहीं रहना पसंद करता है। ग्रामीण मकानों (आवास) के ढाँचों और बनावट में भी परिवर्तन हुआ है।
5. ग्रामीण पुनर्निर्माण पर प्रभाव – नल, सड़क, कुएँ, पंचायतघर, बीज-गोदाम और पशुओं के प्राकृतिक या कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तो हमें आजकल लगभग प्रत्येक गाँव में देखने को मिल जाते हैं। गलियों की सफाई, श्रमदान तथा सड़के बनाना और परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना भी होना प्रारंभ हो गया गया है। किसी-किसी स्थान पर तो समाज कल्याण केंद्र (Social Welfare Centres) की भी स्थापना हो चुकी है, यद्यपि उसका कार्य सीमित है; जैसे–बच्चों के खेल-कूद का प्रबंध आदि। श्रमदान, सर्वोदय और भूदान यज्ञ जैसे आंदोलनों ने ग्रामीण जनता में पुनर्निर्माण की भावनाओं को कुछ आंशिक रूप में परिवर्तित अवश्य किया है।
6. सौंदर्यात्मक और आदर्शात्मक संरचना में परिवर्तन – ग्रामीण समाज में सौंदर्यात्मक और आदर्शात्मक अनुभूतियों में भी परिवर्तन आया है। आज का ग्रामीण व्यक्ति फालतू समय में रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता है। उपन्यास, मनोरंजक कहानियाँ तथा फिल्मी गानों की पुस्तक पढ़ता है और साथ-ही-साथ सिलाई व कढ़ाई-बुनाई की पुस्तकों को पढ़ने में भी अपना समय व्यतीत करता है। ग्रामीण पुरुष और स्त्रियाँ नगरीय पुरुषों और स्त्रियों की वेशभूषा और गहनों की नकल करने लगे हैं इतना ही नहीं, शिक्षित लोगों की ग्रामीण लड़कियाँ और नववधू सौंदर्य के लिए आधुनिक सौंदर्य साधनों का प्रयोग कस्ती हैं। गाँवों में भी लोग आधुनिक प्रकार का फर्नीचर खरीदते हैं। मेहमान के आदर-सत्कार के लिए चाय और कॉफी का प्रयोग करते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि परंपरागत आभूषणों का मोह त्यागकर साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, टेलीविजन, टेपरिकॉर्डर, कैमरा, घड़ी, टार्च, फाउंटेन पैन इत्यादि को रखने में प्रतिष्ठा समझते हैं। घड़ी, फाउंटेन पैन और टेलीविजन तो ग्रामीण अशिक्षित मध्य वर्ग के परिवार में भी आज सामान्य वस्तुएँ समझी जाती है।
उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय ग्रामीण जगत अब प्राचीन ग्रामीण जगत की भाँति नहीं रह गया है। आज का ग्रामीण कूपमंडूक नहीं रहा है तथा वह नगरीय लोगों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।
प्रश्न 12.
गाँव किस प्रकार से नगरों से भिन्न हैं? विस्तार से समझाइए।
या
ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर
चूंकि गाँव ऐक समुदाय है इसलिए इसे अधिकांशत: ग्रामीण सुमदाय ही कहा जाता है। इसी भाँति नगर भी एक समुदाय है तथा इसके लिए नगरीय समुदाय’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर करना एक कठिन कार्य है क्योंकि गाँव की अनेक विशेषताएँ नगरों में पायी जाती हैं, जबकि नगरों की अनेक विशेषताएँ आज गाँव में पायी जाती हैं। फिर भी, दोनों एक नहीं हैं तथा अनेक आधारों पर इनमें अंतर किया जा सकता है।
ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर
ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में निम्नलिखित प्रमुख अंतर पाये जाते हैं –
1. सांस्कृतिक आधार पर अंतर – ग्रामीण समुदाय में कृषि एवं समान उद्योग-धंधों के कारण सभी सदस्यों की संस्कृति समान होती है। नगरीय समुदायों में विभिन्न स्थलों से आकर व्यक्ति बसते हैं अतएव वहाँ सांस्कृतिक असमानता पायी जाती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि ग्रामीण समुदायों में सजातीयता की भावना पायी जाती है, जबकि नगरीय समुदाय में विजातीयता की भावना।
2. सामुदायिक भावना में अंतर – ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना या मिलकर काम करने की भावना पायी जाती है। किंतु नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता के कारण इसका अभाव है।
3. परिवार के आकार में अंतर – ग्रामीण समुदाय में कृषि व्यवस्था के कारण परिवार के आकार बड़े होते हैं और इसमें सामान्यतया संयुक्त परिवार ही पाए जाते हैं, किंतु नगरीय परिवार का आकार छोटा होता है और इसमें एकाकी परिवार पाए जाते हैं।
4. विस्तार में अंतर – ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या कम होती है और नगरीय समुदाय बहुधंधीय होने के कारण जनसंख्या में विस्तृत हो जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण नगरीय समुदाय का विस्तार क्षेत्र अधिक होता है।
5. प्रथाओं मे अंतर – बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, विधवा-पुनर्विवाह निषेध तथा अन्य अनेक प्रकार के विवाह संबंधी निषेध ग्रामीण परिवारों की प्रमुख विशेषताएँ हैं जिनका नगरीय समुदायों में सामान्यतः अभाव होता है।
6. स्त्रियों की स्थिति में अंतर – ग्रामीण समुदाय में स्त्रियों का सामाजिक स्तर नीचा होता है। उन लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। घर की चहारदीवारी में रहकर उन्हें जीवन-यापन करना होता है। नगरीय समुदायों में स्त्रियों का सामाजिक स्तर पुरुषों के समान होता है। उन्हें शिक्षा के अनेक अवसर प्राप्त रहते हैं। पुरुषों के समान वे अनेक क्षेत्रों में भाग लेती हैं।
7. विवाह के आधार में अंतर – ग्रामीण समुदाय में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किंतु नगरीय समुदायों में आजकल प्रेम पर आधारित विवाह संबंध पाए जाते हैं जो अस्थायी होते हैं। नगरीय
समुदायों में विवाह-विच्छेद भी ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा अधिक होता है।
8. संबंधों की प्रकृति में अंतर – ग्रामीण समुदाय के सदस्य एक-दूसरे से परिचित रहते हैं और उनमें अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, किंतु नगरीय समुदाय में संबंधों की औपचारिकता पाई जाती है। नगरीय समुदायों में परिवार के सदस्यों में भी औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। इन्हीं औपचारिक संबंधों के कारण नगरीय जीवन अलगावकृत होता जा रहा है।
9. पड़ोसीपन की भावना में अंतर – ग्रामीण समुदाय में पड़ोस व जाति का विशेष महत्त्व है। नगरों में प्रायः दोनों ही प्रभावहीन हैं। अवैयक्तिक तथा अनौपचारिक संबंधों के कारण नगरों में आज पड़ोसियों में भी अनजानापन देखा जा सकता है। महानगरों में तो कई बार पड़ोसी एक-दूसरे से पूरी तरह परिचित तक नहीं होते।
10. मनोरंजन के साधन में अंतर – ग्रामीण समुदायों में परिवार ही मनोरंजन के साधन हैं, किंतु नगरीय समुदाय में सिनेमाघर, क्लब आदि व्यावसायिक मनोरंजन के केंद्र हैं। नगरों में मनोरंजन
भी एक व्यवसायी बन गया है।
11. व्यक्तियों की सुविधाओं में अंतर – ग्रामीण समुदायों में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है; किंतु नगरीय समुदायों में अनेक समितियों, सभाओं तथा संगठनों द्वारा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होता है। ग्रामीण समुदायों में सुविधाओं का अभाव पाया जाता है जिसके कारण ग्रामवासियों में संकीर्णता की भावना बनी रहती है। नगरीय समुदायों में अत्यधिक सुविधाओं के कारण जीवन का स्तर उच्च होता है तथा समाजिक गतिशीलता भी अधिक पायी जाती है।
12. विचारों में अंतर – ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों में विचारों में संकीर्णता पायी जाती हैं, किंतु नगरीय समुदाय में रेडियो, समाचार-पत्रों एवं विविध प्रकार की उपसंस्कृतियों के कारण विचारों में व्यापकता अधिक होती है। वस्तुत: नगरीय जीवन में इतनी अधिक विविधता पायी जाती है कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक ही है।
13. सामाजिक नियंत्रण में अंतर – ग्रामीण समुदाय में परिवार, पड़ोस, प्रथाएँ, रीति-रिवाज, धर्म तथा जाति पंचायत सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अनौपचारिक साधन हैं, जबकि नगरों में पुलिस तथा कानून ही सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण के औपचारिक साधन है। नगरों में अनौपचारिक साधन इतने अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होते जितने कि वे ग्रामीण समुदाय में होते हैं।
14. सामाजिक जीवन में अंतर – ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति का जीवन सरल, पवित्र तथा परंपरावादी होता है। अतएव व्यक्ति बुराइयों से बचा रहता है। किंतु नगरीय समाज का व्यक्ति जुआ, शराब आदि का शिकार हो जाता है अतएव नगरीय समुदायों में अपराधों की संख्या बढ़ती है और वैयक्तिक तथा पारिवारिक अथवा सामाजिक विघटन अधिक होते हैं।
निष्कर्ष – उपर्युक्त विवचेन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय दो भिन्न अवधारणाएँ हैं। इनमें विविध आधारों पर अंतर किया जा सकता है। आज दोनों प्रकार के समुदायों में इतनी अधिक अंत:क्रिया हो गई है कि दोनों में अंतर करना कठिन होता जा रहा है।

प्रश्न 13.
नगरीय समाज के परिवर्तित प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए।
या
नगरीय समाज में हो रहे परिवर्तनों की स्पष्ट रूप से विवेचना कीजिए।
उत्तर
नगरीय समाज की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन हैं। नगरीय समाज की परिभाषा विद्वानों ने जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। हेलबर्ट (Helbert) के अनुसार, “स्वयं सभ्यता के जन्म के समान ही नगर का जन्म भी भूत के अँधेरे में सो गया है।” किंग्स्ले डेविस (Kingsley Davis) का कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार के वातावरण अर्थात् नगरीय परिस्थितियों की उपज होती है। इनके अनुसार, “नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पायी जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है।”
नगरीय समाज में हो रहे प्रमुख परिवर्तन
नगरीय समाज में हो रहे प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं –
1. सहिष्णुता – नगरीय समाज के लोगों में रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान की विषमता पायी जाती है किंतु फिर भी लोग ऐसा जीवन बनाए रखते हैं कि वे एक-दूसरे की बातों को सहन
करते हैं। इससे सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिलता है।
2. विषमता में वृद्धि – नगरीय समाज के लोगों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में समरूपता नहीं पायी जाती है। नगरों में विभिन्न रीति-रिवाज, विचारों, व्यवसायों तथा संस्कृतियों के लोग एकत्र होते हैं जिससे उनमें विषमता आती है। अत: नगरीय समाज अत्यधिक विजातीयता वाले समुदाय होते जा रहे हैं जिससे विभिन्न समूहों में संघर्ष की स्थिति भी विकसित हो रही है।
3. नियंत्रण में शिथिलता – नगरों में कानून जैसे औपचारिक साधनों व द्वितीयक समूहों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण में सुव्यवस्था कम ही मात्रा में स्थापित हो सकती है। नगरों में नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का महत्त्व समाप्त हो जाता है जिससे नियंत्रण में शिथिलता आ जाती है।
4. अप्रत्यक्ष संपर्क में वृद्धि – नगरीय समाज में लोगों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं होती तथा उनमें प्रायः अप्रत्यक्ष संबंध पाये जाते हैं। इसका मुख्य कारण नगरों की जनसंख्या है। वास्तव में, जनसंख्या ही इतनी अधिक होती है कि सभी में प्रत्यक्ष संबंध हो ही नहीं सकते हैं। अप्रत्यक्ष संबंधों के कारण ही प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण संभव नहीं रह पाता।
5. सामाजिक गतिशीलता – यातायात के साधनों में विकास होने के कारण नगर के निवासी एक | स्थान से दूसरे स्थान को आते-जाते रहते हैं। वे आजीविका या व्यवसाय की खोज में भी इधर-उधर घूमते रहते हैं। समाज की प्रथाओं में परिवर्तन करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता है। अतएव नगरों में सामाजिक गतिशीलता का गुण पाया जाता है।
6. व्यक्तित्व का विकास – नगरों में व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार पद प्राप्त कर सकता है तथा अपना विकास कर सकता है। गतिशीलता के अधिक अवसर होने के कारण तथा अर्जित गुणों
की महत्ता के कारण व्यक्तित्व का विकास इच्छानुसार हो सकता है।
7. समस्याओं में वृद्धि – नगरों में विविध प्रकार की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन समस्याओं में बाल अपराध, अपराध, श्वेतवसन, अपराध, भ्रष्टाचार, मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, निर्धनता एवं बेरोजगारी इत्यादि प्रमुख हैं।
8. ऐच्छिक संपर्क – नगरों में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चाहे जिसके साथ संपर्क स्थापित करे या न करे। ऐच्छिक संपर्क के कारण ही नगरों में ऐच्छिक समितियों की संख्या बढ़ने लगी है।
9. व्यक्तिवादिता – नगरों में व्यक्ति स्वार्थ की ओर ही ध्यान देता है, अतएव नगरों में सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता पायी जाती है। नगरीय जीवन इतना व्यस्त है कि लोगों को दूसरों के सुख-दु:ख में हिस्सा लेने का समय ही नहीं मिलता। परिवार के सदस्यों तक में व्यक्तिवाद की भावना विकसित होने लगती है।
We hope the UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 11 Sociology Understanding Society Chapter 2 Social Change and Social Order in Rural and Urban Society (ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.