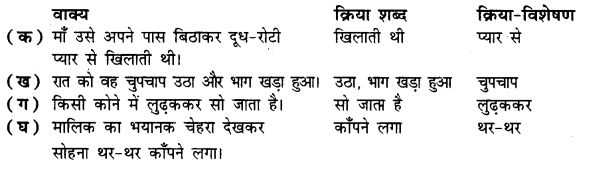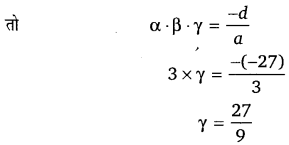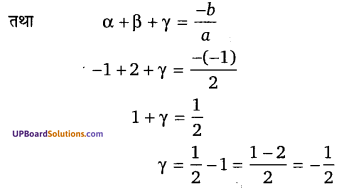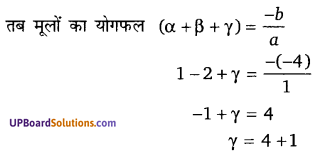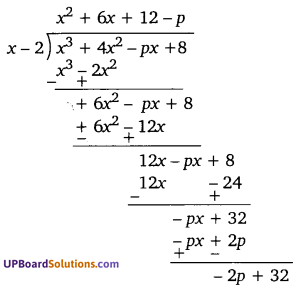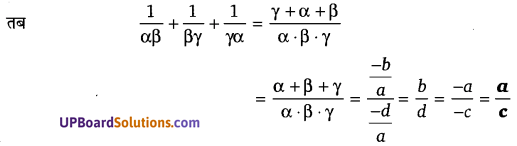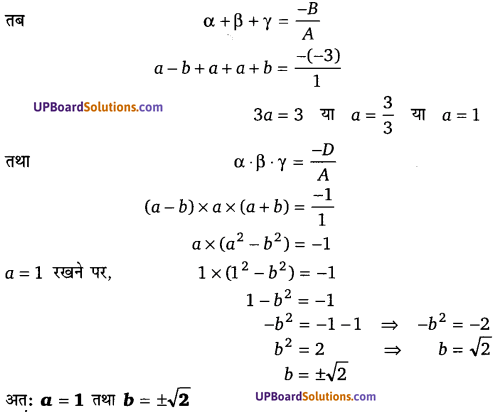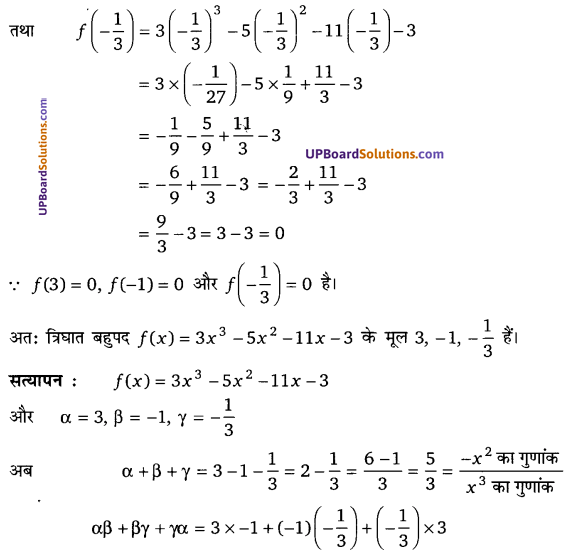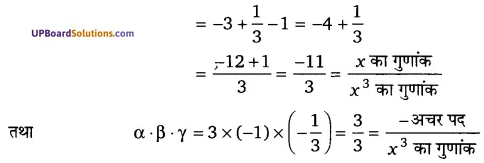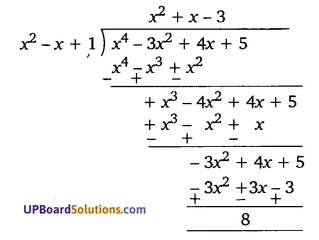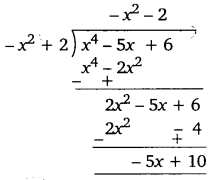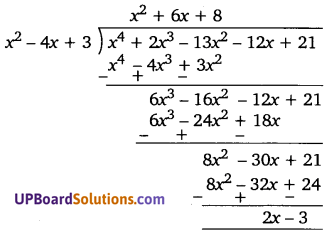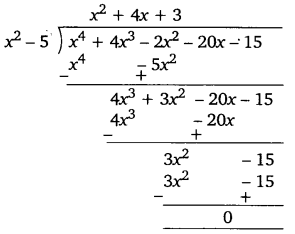UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 1 The Cold War Era (शीतयुद्ध का दौर)
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 Text Book Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1.
शीतयुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(क) यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी।
(ख) यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था।
(ग) शीतयुद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की।
(घ) अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे।
उत्तर:
(घ) अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे।
प्रश्न 2.
निम्न में से कौन-सा कथन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता?
(क) उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतन्त्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना।
(ख) किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार करना।
(ग) वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना।
(घ) वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केन्द्रित करना।
उत्तर:
(ग) वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना।

प्रश्न 3.
नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिह्न लगाएँ
(क) गठबन्धन के सदस्य देशों को अपने भू-क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था।
(ख) सदस्य देशों को विचारधारा और राजनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था।
(ग) जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य-देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था।
(घ) महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थीं।
उत्तर:
(क) गठबन्धन के सदस्य देशों को अपने भू-क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। (सही)
(ख) सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। (सही)
(ग) जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। (सही)
(घ) महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थीं। (गलत)
प्रश्न 4.
नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीतयुद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था?
(क) पोलैण्ड
(ख) फ्रांस
(ग) जापान
(घ) नाइजीरिया
(ङ) उत्तरी कोरिया
(च) श्रीलंका
उत्तर:
(क) पोलैण्ड–साम्यवादी गुट (सोवियत संघ)।
(ख) फ्रांस-पूँजीवादी गुट (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
(ग) जापान–पूँजीवादी गुट (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
(घ) नाइजीरिया-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।
(ङ) उत्तरी कोरिया-साम्यवादी गुट (सोवियत संघ)।
(च) श्रीलंका-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।
प्रश्न 5.
शीतयुद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियन्त्रण ये दोनों ही प्रक्रियाएँ पैदा हुईं। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे?
उत्तर:
शीतयुद्ध के दौरान पूँजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिद्वन्द्विता समाप्त नहीं हुई थी। इसी वजह से परस्पर अविश्वास की परिस्थितियों में दोनों गठबन्धनों ने हथियारों का भारी भण्डारण करते हुए लगातार युद्ध की तैयारियाँ की। दोनों ही गुट अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु हथियारों के बड़े जखीरे को आवश्यक समझते थे। चूँकि दोनों ही गुट परमाणु हथियारों से लैस थे तथा वे इसके प्रयोग के दुष्परिणामों से भली-भाँति परिचित भी थे। दोनों महाशक्तियाँ जानती थीं कि यदि प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा गया तो दोनों को भारी नुकसान होगा और इनमें से किसी के भी विश्व विजेता बनने की सम्भावनाएँ काफी कम हैं। अत: दोनों महाशक्तियों ने हथियारों पर नियन्त्रण के लिए अस्त्र-शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के प्रयास किए।

प्रश्न 6.
महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबन्धन क्यों रखती थीं? तीन कारण बताइए।
उत्तर:
छोटे देशों के साथ महाशक्तियों द्वारा सैन्य गठबन्धन रखने के प्रमुख रूप से निम्नांकित तीन कारण थे
- महत्त्वपूर्ण संसाधन हासिल करना-महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता था।
- भू-क्षेत्र–महाशक्तियाँ इन छोटे देशों को अपने हथियारों की बिक्री करती थीं और इनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सेना का संचालन करती थीं।
- सैनिक ठिकाने-छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने बनाकर दोनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे की जासूसी करती थीं।
प्रश्न 7.
कभी-कभी कहा जाता है कि शीतयुद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं था।क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दें।
उत्तर:
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ-संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ का आविर्भाव हुआ, जो कि अलग-अलग विचारधारा वाले थे। ऐसे में किसी भी देश के लिए एकमात्र विकल्प यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे।
शीतयुद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था इसका विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं था, इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि विश्व के साम्यवादी विचारधारा वाले, सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए और पश्चिमी देश जो कि पूँजीवादी विचारधारा के थे, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल हुए। सन् 1941 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया।
प्रश्न 8.
शीतयुद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया?
उत्तर:
स्वतन्त्रता के पश्चात् तथा शीतयुद्ध के अन्त (1991) तक भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति अलग-अलग रही।
भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के कारण प्रारम्भ से ही अमेरिका भारत से नाराज रहा और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमन्त्री के रूप में कार्यकाल से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं चन्द्रशेखर के प्रधानमन्त्री के रूप में कार्यकाल तक (शीतयुद्ध की समाप्ति तक) अमेरिका के साथ भारत के विशेष सम्बन्ध नहीं रहे। हालाँकि इस दौरान समय-समय पर अमेरिका ने भारत के साथ सम्बन्धों में थोड़ा-बहुत सुधार अवश्य किया, परन्तु वह पाकिस्तान को निरन्तर सैन्य सहायता देता रहा, यद्यपि अमेरिका ने पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ की निन्दा की, परन्तु इसके पीछे भी उसकी सोची-समझी कूटनीतिक चाल थी।
शीतयुद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध मधुर रहे। भारत और सोवियत संघ निरन्तर एकदूसरे को सहयोग करते रहे। सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर ‘भारत महोत्सव’ का आयोजन किया गया।
भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया। इस नीति के कारण भारत ऐसे निर्णय ले सका जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके हितों की पूर्ति हो सकी। साथ ही वह सदैव ऐसी स्थिति में रहा कि यदि कोई एक महाशक्ति उसका अथवा उसके हितों का विरोध करे तो दूसरी महाशक्ति उसको सहयोग करती। स्पष्ट है कि शीतयुद्ध के दौरान भारत अपने हितों के लिए लगातार सजग रहा।
प्रश्न 9.
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीतयुद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुँचाई?
उत्तर:
शीतयुद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वन्द्वी गुटों में बाँटा हुआ था। इसी सन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव-स्वतन्त्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय यह नहीं है कि इस आन्दोलन से जुड़े देश अपने को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से अलग-थलग रखते हैं अथवा तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है-पृथकतावाद नहीं। तीसरी दुनिया के देशों के विकास में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने विशेष भूमिका निभायी।
संक्षेप में इस तथ्य को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-
(1) गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल अधिकांश देशों को ‘अल्प विकसित देश’ का दर्जा मिला हुआ था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से अधिक विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी।
(2) इसी दृष्टिकोण से नव-आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। सन् 1912 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से सम्बन्धित सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया था कि सुधारों से-
(क) अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं।
(ख) अल्प विकसित देशों की पहुँच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमन्द होगा।
(ग) पश्चिमी देशों से मँगाई जा रही प्रौद्योगिकी की मात्रा कम होगी और
(घ) अल्प विकसित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी।
(3) गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे-धीरे बदली और इसमें आर्थिक गुटों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा।
(4) बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन (1961) में आर्थिक मुद्दे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं थे।
1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके कारण गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया।
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में तथा सभी नव-स्वतन्त्र देशों को अपनी-अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में इस गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया।

प्रश्न 10.
“गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अब अप्रासंगिक हो गया।” आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर:
गुटनिरपेक्षता की नीति शीतयुद्ध के सन्दर्भ में सामने आई थी। शीतयुद्ध के अन्त और सोवियत संघ के विघटन से एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में कमी आयी।
सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एकध्रुवीय बन चुका है। सन् 1992 में इण्डोनेशिया में दसवें शिखर सम्मेलन में अधिकतर सदस्यों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को जारी रखने के साथ-साथ इसके उद्देश्यों को परिवर्तित करने पर जोर दिया।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की वर्तमान प्रासंगिकता
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की वर्तमान प्रासंगिकता को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-
- गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएँ तो एक शक्ति बन सकते हैं।
- गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण किसी भी गरीब और छोटे देश को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है।
- कोई भी देश अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति अपना सकता है।
- गुटनिरपेक्ष देशों को आज भी आपसी सहयोग की दृष्टि से इस मंच की आवश्यकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए इन निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग आवश्यक है।
- यह नीति आज भी गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है साथ ही विश्व में नि:शस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देती है।
- वास्तव में गुटनिरेपक्ष आन्दोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतन्त्रधर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अतः शीतयुद्ध के बाद भी यह आन्दोलन प्रासंगिक है।
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 InText Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 पाठान्तर्गत प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट से कम-से-कम तीन देशों की पहचान करें।
उत्तर:
सोवियत संघ गुट के तीन सदस्य थे—
- पोलैण्ड,
- पूर्वी जर्मनी और
- रोमानिया।
अमेरिकी गुट के तीन सदस्य थे-
- पश्चिमी जर्मनी,
- ब्रिटेन और
- फ्रांस।
प्रश्न 2.
पाठ्यपुस्तक के अध्याय चार में दिए गए यूरोपीय संघ के मानचित्र को देखें और उन चार देशों के नाम लिखें जो पहले ‘वारसा सन्धि’ के सदस्य थे और अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं।
उत्तर:
- रोमानिया,
- बुल्गारिया,
- हंगरी,
- पोलैण्ड।
प्रश्न 3.
इस मानचित्र की तुलना यूरोपीय संघ के मानचित्र तथा विश्व के मानचित्र से करें। इस तुलना के बाद ऐसे तीन देशों के नाम लिखिए जो शीतयुद्ध के बाद अस्तित्व में आए।

उत्तर:
- उक्रेन,
- कजाकिस्तान,
- किरगिस्तान, तथा
- बेलारूसा (कोई तीन)
प्रश्न 4.
निम्नलिखित तालिका में तीन-तीन देशों के नाम उनके गुटों को ध्यान में रखकर लिखें-पूँजीवादी गुट, साम्यवादी गुट और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।
उत्तर:
पूँजीवादी गुट–
- संयुक्त राज्य अमेरिका,
- ब्रिटेन,
- फ्रांस।
साम्यवादी गुट–
- सोवियत संघ,
- पोलैण्ड,
- हंगरी।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन–
- भारत,
- मिस्र,
- घाना।
प्रश्न 5.
उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक क्यों विभाजित हैं जबकि शीतयुद्ध के दौर के बाकी विभाजन मिट गए हैं? क्या कोरिया के लोग चाहते हैं कि विभाजन बना रहे?
उत्तर:
उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक विभाजित हैं क्योंकि इसके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के हित निहित हैं। इसलिए यहाँ के शासक वर्ग कोरिया के एकीकरण की ओर कदम नहीं बढ़ा पाए हैं। यद्यपि कोरिया के लोग विभाजन नहीं चाहते।

प्रश्न 6.
पाँच ऐसे देशों के नाम बताएँ जो दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए।
उत्तर:
- भारत,
- पाकिस्तान,
- घाना,
- इण्डोनेशिया,
- मिस्र।
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 Other Important Questions
UP Board Class 12 Civics Chapter 1 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
क्यूबा मिसाइल संकट पर विस्तार से लेख लिखिए।
उत्तर:
क्यूबा का मिसाइल संकट क्यूबा, अन्ध महासागर में स्थित एक छोटा-सा द्वीपीय देश है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय सीमा के निकट है। क्यूबा के मिसाइल संकट को निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-
1. क्यूबा का सोवियत संघ से लगाव-क्यूबा का अपने समीपवर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा सोवियत संघ से लगाव था क्योंकि क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था। सोवियत संघ उसे कूटनयिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता था।
2. सोवियत संघ के नेताओं की चिन्ता-अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिन्ता सता रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूँजीवादी देश है जो विश्व में साम्यवाद को पसन्द नहीं करता। अत: वह साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति के आगे एक शक्तिहीन देश है।
3. क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करना-सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर आक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय किया। सन् 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका का नजदीकी निशाने की सीमा में आना-सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती से पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। मिसाइलों की तैनाती के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो गयी।
सोवियत संघ पहले की तुलना में अब संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भू-भाग के लगभग दुगुने ठिकानों अथवा शहरों पर हमला कर सकता था।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को चेतावनी दिया जाना—क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग तीन सप्ताह बाद प्राप्त हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी व उनके सलाहकार दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे; फलस्वरूप उन्होंने संयम से काम लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी चाहते थे कि खुश्चेव क्यूबा से परमाणु मिसाइलों व अन्य हथियारों को हटा लें। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाजों को रोकें, इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गम्भीरता की चेतावनी देना चाहता था। इस तनावपूर्ण स्थिति से ऐसा लगने लगा कि दोनों महाशक्तियों के मध्य भयानक युद्ध निश्चित रूप से होगा। सम्पूर्ण विश्व चिन्तित हो गया। इसे ही ‘क्यूबा मिसाइल संकट’ के नाम से जाना गया।
6. दोनों महाशक्तियों द्वारा युद्ध को टालने का फैसला-संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने युद्ध की भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध को टालने का फैसला लिया। दोनों पक्षों के इस फैसले से समस्त विश्व ने चैन की साँस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली अथवा वापसी का रुख कर लिया।
इस तरह क्यूबा का मिसाइल संकट टल गया, लेकिन इसने दोनों महाशक्तियों के मध्य शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया जो सोवियत संघ के विघटन तक जारी रहा।
प्रश्न 2.
शीतयुद्ध से क्या अभिप्राय है? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर शीतयुद्ध के प्रभाव को विस्तार से बताइए।
उत्तर:
शीतयुद्ध से अभिप्राय शीतयुद्ध से अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह स्थिति शीतयुद्ध के नाम से जानी जाती है।
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर शीतयुद्ध का प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति) पर शीतयुद्ध के अनेक प्रभाव पड़े, जिनको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों से बाँटा जा सकता है- शीतयुद्ध के सकारात्मक प्रभाव-
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर शीतयुद्ध के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं-
1.शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन दोनों महाशक्तियों के मध्य शीतयुद्ध की भयावहता के कारण . सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला।
2. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति-दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ में शीतयुद्ध के कारण सम्पूर्ण विश्व दो प्रतिद्वन्द्वी गुटों में बँट रहा था। इन दोनों गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का जन्म एवं विकास हुआ जिसके तहत तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन कर सके।
3. नव-अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प-विकसित देश का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती अपने देश का आर्थिक विकास करना था। बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही अर्थों में स्वतन्त्र नहीं रह सकता था, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था, जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई। इसी सोच के कारण नव-अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ।
4. प्रौद्योगिक विकास-शीतयुद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला।
(II) शीतयुद्ध के नकारात्मक प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर शीतयुद्ध के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं-
1. विश्व का दो गुटों में विभाजन-शीतयुद्ध के कारण विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो गया तो दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया। इन गुटों के निर्माण से दोनों गुटों में सम्मिलित देशों को अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति के साथ समझौता करना पड़ा तथा जो किसी गुट में । सम्मिलित नहीं हुए; उन पर अपने गुट में सम्मिलित होने हेतु दोनों महाशक्तियों द्वारा दबाव डाला गया।
2. सैन्य गठबन्धनों का उद्भव-शीतयुद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक सैन्य गठबन्धनों का उद्भव हुआ।
3. शस्त्रीकरण को बढ़ावा-शीतयुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह नकारात्मक प्रभाव डाला कि इसके कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। .
4. निःशस्त्रीकरण की असफलता-शीतयुद्ध के निरन्तर तनाव भरे वातावरण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। अस्त्र-शस्त्रों की होड़ ने इसे अप्रभावी बना दिया।
5. भय तथा सन्देह के वातावरण का जन्म-शीतयुद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और सन्देह के वातावरण का जन्म हुआ जो शीतयुद्ध की समाप्ति तक निरन्तर बना रहा।
6. परमाणु युद्ध का भय-द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था इसी होड़ के कारण सोवियत संघ ने भी परमाणु अस्त्रों का विकास किया। इससे यद्यपि दोनों महाशक्तियों के मध्य शान्ति सन्तुलन स्थापित हुआ, लेकिन उनके बीच सैन्य स्पर्धा भी अत्यधिक बढ़ने लगी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय समस्त विश्व को यह लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु युद्ध अवश्यम्भावी है, लेकिन यह संकट टल गया।
प्रश्न 3.
शीतयुद्ध के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर.
शीतयुद्ध के उदय के प्रमुख कारण शीतयुद्ध के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
1. परस्पर सन्देह एवं भय-दोनों गुटों के देशों के मध्य शीतयुद्ध का कारण परस्पर सन्देह, अविश्वास तथा डर का व्याप्त होना था क्योंकि पाश्चात्य देश बोल्शेविक क्रान्ति से काफी भयभीत हुए थे जिसने आपस में अविश्वास तथा भय की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया था।
2. विरोधी विचारधारा-दोनों महाशक्तियों के अनुयायी देश परस्पर विरोधी विचारधारा वाले थे। जहाँ एक पूँजीवादी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था वाला देश था वहीं दूसरा साम्यवादी विचारधारा से ओत-प्रोत था। विश्व में दोनों ही अपना-अपना प्रभुत्व अधिकाधिक क्षेत्र पर स्थापित करना चाहते थे।
3. जर्मनी का घटनाक्रम-द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बँट गया। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता सँभाली जबकि पश्चिमी हिस्से में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की साम्यवादी विरोधी शक्तियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। इस कारण से स्थितियाँ निरन्तर तनावपूर्ण होती चली गईं।
4. माल्टा समझौते की अवहेलना-शीतयुद्ध के उदय का एक अन्य कारण यह भी था कि सोवियत संघ माल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा था तथा वह पोलैण्ड में साम्यवादी सरकार स्थापित करने में मददगार साबित हो रहा था।
5. पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार–पाश्चात्य देशों ने सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान जोर-शोर से चला रखा था। इसके पीछे इनका यह उद्देश्य था कि पश्चिम के अधिक-से-अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध इकट्ठे हो जाएँ और सोवियत संघ अलग-थलग पड़कर अकेला हो जाए।
6. सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार-सोवियत संघ ने भी प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे कार्य किए जिनसे शीतयुद्ध के बादल और गहराते चले गए।
7. शान्ति समझौते पर परस्पर मतभेद-दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ और पाश्चात्य देशों के बीच अनेक बातों पर एक अभिमत नहीं था। उदाहरणार्थ; इटली तथा यूगोस्लाविया का सीमा सम्बन्धी मामला। सोवियत संघ, लीबिया को अपने संरक्षण में लेना चाहता था और इटली से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का आकांक्षी भी था लेकिन ये सभी बातें पाश्चात्य देशों को नापसन्द थीं। इस प्रकार निरन्तर बढ़ते मतभेदों से शीतयुद्ध का मार्ग खुल रहा था।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति-द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों में अविश्वास तथा तनाव की चौड़ी खाई को पाटने में असफल सिद्ध हुआ।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग–पाश्चात्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी संख्यात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया लेकिन सोवियत संघ ने पश्चिमी गुट की एक न चलने दी और उसके खिलाफ अनेक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य पाश्चात्य देशों ने भी सोवियत संघ विरोधी कार्यों को क्रियान्वित किए जाने की एक मुहिम-सी छेड़ दी।
10. अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से छिपाना-शीतयुद्ध के उदय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट-ब्रिटेन ने अणु बमों के अनुसन्धान को सोवियत संघ से छिपाकर रखा। सोवियत संघ को इनकी इस कपटपूर्ण चालाकी (चतुराई) से काफी ठेस पहुंची। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच सम्बन्धों में कभी न भरी जाने वाली दरार पैदा हो गई।

प्रश्न 4.
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका को समझाते हुए आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
उत्तर:
गुटनिरपेक्षता का अर्थ गुटनिरपेक्षता का अर्थ है—दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने तथा अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाते हुए विश्व राजनीति में शान्ति और स्थिरता के लिए सक्रिय रहने का आन्दोलन है। न यह तटस्थता है और न पृथक्तावाद। अतः गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय हित एवं विश्वशान्ति के आधार पर गुटों से अलग रहते हुए निर्णय लेने की स्वतन्त्रता।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर प्रमुख थे। इण्डोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूना ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पाँच नेता गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक कहलाए।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है-
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक-भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया।
- स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबन्दी से अलग रखा-शीतयुद्ध के दौर में भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबन्दी से दूर रखा।
- नव-स्वतन्त्र देशों को आन्दोलन में आने के लिए प्रेरित किया—भारत ने नव-स्वतन्त्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया तथा उनके समक्ष तीसरा विकल्प प्रस्तुत करके उन्हें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित किया।
- विश्वशान्ति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को सक्रिय रखना-भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर बल दिया।
- वैचारिक एवं संगठनात्मक ढाँचे का निर्धारण-गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के वैचारिक एवं संगठनात्मक ढाँचे के निर्धारण में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- समन्वयकारी भूमिका-भारत ने समन्वयकारी भूमिका निभाते हुए सदस्यों के बीच उठे विवादास्पद मुद्दों को टालने या स्थगित करने पर बल देकर आन्दोलन को विभाजित होने से बचाया।
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक विवेचन
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है-
(I) भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के लाभ
गुटनिरपेक्षता की नीति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है-
1. राष्ट्रीय हित के अनुरूप फैसले-गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता था, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का।
2. अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपने महत्त्व को बनाए रखने में सफल-गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत सरकार को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही दबाव डाल सकता था।
(II) भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की निम्नलिखित कारणों से आलोचना की गई है-
1. सिद्धान्त विहीन नीति-भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धान्त विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्त्वपूर्ण मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है।
2. अस्थिर नीति–भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति में अस्थिरता रही है।
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
शीतयुद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
शीतयुद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव
- विश्व का दो गुटों में विभाजन-शीतयुद्ध का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व दो खेमों में विभक्त हो गया। एक खेमा पूँजीवादी गुट कहलाया और दूसरा साम्यवादी गुट कहलाया।
- सैनिक गठबन्धनों की राजनीति-शीतयुद्ध के कारण सैनिक गठबन्धनों की राजनीति प्रारम्भ हुई।
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति-शीतयुद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति हुई। एशिया-अफ्रीका के नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों ने दोनों गुटों से अपने को अलग रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का हिस्सा बनना उचित समझा।
- शस्त्रीकरण को बढ़ावा-शीतयुद्ध का एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव यह पड़ा कि इससे शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। दोनों गुट खतरनाक शस्त्रों का संग्रह करने लगे।
प्रश्न 2.
शीतयुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों पर अपना नियन्त्रण क्यों बनाए रखना चाहती थीं? अथवा महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबन्धन बनाए रखने को क्यों प्रेरित थीं?
उत्तर:
(1) शीतयुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों पर अपना नियन्त्रण बनाए रखने के कारण-
(2) महत्त्वपूर्ण संसधानों को हासिल करना-महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता था।
(3) भू-क्षेत्र-महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के यहाँ अपने हथियारों की बिक्री करती थीं और इनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सेना का संचालन करती थीं।
सैन्य ठिकाने-छोटे देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाकर दोनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे गुट की जासूसी करती थीं।
(4) छोटे देश विचारधारा की वजह से भी महाशक्तियों के लिए महत्त्वपूर्ण थे। गुटों में सम्मिलित देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुटों में सम्मिलित हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थीं कि उदारवादी लोकतन्त्र तथा पूँजीवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद से अधिक श्रेष्ठ है अथवा समाजवाद एवं साम्यवाद, उदारवादी लोकतन्त्र तथा पूँजीवाद की अपेक्षा बेहतर है।
प्रश्न 3.
शीतयुद्ध के काल में अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो रोका लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता को क्यों नहीं रोक सकी?
उत्तर:
शीतयुद्ध काल में अवरोध की स्थिति महाशक्तियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता को निम्नलिखित कारणों से रोकने में असफल रही-
(1) महाशक्तियों से जुड़े देश यह जानते थे कि परस्पर युद्ध अत्यन्त ही खतरों से भरा हुआ है क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रयोग किए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बमों का भारी भण्डारण था।
(2) आपसी प्रतिद्वन्द्विता न रुक पाने का एक अन्य कारण दोनों महाशक्तियों की अलग-अलग तथा विपरीत विचारधारा थी। पृथक्-पृथक् विचारधाराएँ होने के कारण उनमें कोई समझौता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था।
(3) दोनों महाशक्तियाँ औद्योगीकरण के चरम विकास की अवस्था में थीं और उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल विश्व के अल्प विकसित देशों से ही प्राप्त हो सकता था। एक प्रकार से यह उन देशों के लिए की गई छीना-झपटी अथवा प्रतिस्पर्धी थी।
प्रश्न 4.
1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
1960 के दशक को खतरनाक दशक कहे जाने के कारण-
- सन् 1958 में बार्लिन की दीवार के निर्माण की वजह से जर्मन, शेष यूरोप तथा महाशक्तियों के नेतृत्व में विभक्त विश्व के दोनों गुटों में तनाव और अधिक बढ़ा।
- 1960 के दशक के प्रारम्भ में ही कांगो सहित अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो गई। यह संकट और अधिक विकराल होता चला गया क्योंकि दोनों गुटों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने हेतु सहमत नहीं था।
- 1960 के दशक में कोरिया, वियतनाम तथा अफगानिस्तान इत्यादि में व्यापक स्तर पर जनहानि हुई थी। अनेक बार महाशक्तियों के बीच राजनीतिक वार्ताएँ भी नहीं हुईं जिससे दोनों के बीच गलतफहमियों की खाई और गहरी हो गई।
- सन् 1962 तथा 1965 में भारत पर क्रमश: चीन तथा पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया।
- सन् 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित ‘बे ऑफ पिग्स’ आक्रमण किया गया।
- सन् 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई।
- सन् 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था।
प्रश्न 5.
“गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्विध्रुवीय विश्व के समक्ष चुनौती था।” इस कथन को न्यायोचित ठहराइए।
उत्तर:
उक्त कथन को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सकता है-
- विश्व की दोनों महाशक्तियाँ नव-स्वतन्त्रता प्राप्त तीसरे विश्व के अल्पमत विकसित देशों को लालच देकर दबाव बनाकर तथा समझौतों का प्रलोभन देकर उनको अपने-अपने गुट में मिलाने हेतु लालायित थे।
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक सदस्यों में एशिया के पं० जवाहरलाल नेहरू तथा सुकर्णो तथा अफ्रीका के वामे एनक्र्मा थे। ये सभी तीसरी दुनिया के प्रतिनिधि देश थे और इन्होंने परतन्त्रता का स्वाद चखा था।
- शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा पश्चिम के अनेक देशों पर हमले किए गए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को अनवरत चलाए रखना स्वयं में काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। ।
- पाँच सदस्य देशों से अपना सफर शुरू करने वाले गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी सदस्य संख्या 120 कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में अपने समर्थक बनाना भी अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है।
प्रश्न 6.
शीतयुद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका किस प्रकार जिम्मेदार था?
उत्तर:
शीतयुद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका निम्नलिखित कारणों से जिम्मेदार था-
- अणु बम का रहस्य गुप्त रखना-अमेरिका ने अणु बम के रहस्य को सोवियत संघ से गुप्त रखा। इस बात से क्षुब्ध होकर सोवियत संघ अस्त्र-शस्त्र बनाने में लग गया तथा कुछ ही वर्षों में अणु बम का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो दोनों में शस्त्रास्त्रों की होड़ लग गई।
- रूस विरोधी प्रचार-युद्ध काल में ही पश्चिमी देशों के सूचना प्रसार के संसाधन रूस विरोधी प्रचार करने लग गए थे। बाद में इन देशों ने खुले आम सोवियत संघ की आलोचना करनी आरम्भ कर दी। उसके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का यह प्रचार शीतयुद्ध को बढ़ावा देने का कारण बना।
- अमेरिका का जापान पर अधिकार ज़माने का कार्यक्रम-जापान पर अमेरिका द्वारा अणु बम के प्रयोग के बाद रूस को शक हो गया कि अमेरिका जापान पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता है। इससे दोनों देशों में तनाव हो गया।
प्रश्न 7.
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को अनियमित’ तथा ‘सिद्धान्तहीन’ कहा जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं, क्यों?
उत्तर:
यह विचार ‘असहमत’ होने योग्य है। आलोचकों द्वारा एकपक्षीय अवलोकन करके ही गुटनिरपेक्ष नीति पर उक्त टिप्पणी की गई है। सन् 1971 में बंगलादेश युद्ध के समय पाकिस्तान को चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियार और आर्थिक सहायता दिए जाने की वजह से भारत की अस्मिता तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर संकट उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान मामले में हस्तक्षेप करने वाली एक साम्यवादी तथा दूसरी पूँजीवादी शक्ति की इस कुचेष्टा को निरुत्साहित करने के लिए भारत का सोवियत संघ के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वथा उचित था।
गुटनिरपेक्षता की नीति इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थी कि दो महाशक्तियाँ नए आजाद हुए देशों की सम्प्रभुता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के किसी भी सदस्य देश को ऐसी विषम परिस्थिति में कूटनीति अपनाने से कभी भी नहीं रोका तथा इसके विपरीत सहायता ही उपलब्ध कराई। दक्षिण एशिया का ‘आसियान’ संगठन भी गुटनिरपेक्ष नीति का ही एक रूप है।
प्रश्न 8.
गुटनिरपेक्षता क्या है? क्या गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता है?
उत्तर:
गुटनिरपेक्षता का अर्थ है महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिले न होना अर्थात् इन गुटों के सैन्य गठबन्धनों व सन्धियों से अलग रहना तथा गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व राजनीति में भाग लेना।
गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है-गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। तटस्थता का अभिप्राय है-युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ऐसे देश न तो युद्ध में संलग्न होते हैं और न ही युद्ध के सही-गलत के सम्बन्ध में अपना कोई पक्ष रखते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्षता युद्ध को टालने तथा युद्ध के अन्त का प्रयास करने की नीति है।

प्रश्न 9.
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
उत्तर:
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य-
- विश्व की अर्थव्यवस्था की अन्त:निर्भरता का अधिक कुशलता एवं न्यायपूर्ण प्रबन्धन हो।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो जिससे विकासशील देशों को अधिकाधिक फायदा मिल सके।
- विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नवीन प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगी व्यापारिक रुकावटों को हटाया जाए और वस्तुओं का निर्यात करने में विकासशील देशों को अधिक अनुकूल शर्ते प्रदान की जाएँ।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार-संहिता लागू की जाए।
- विकसित देश विकासशील देशों में अपनी पूँजी का निवेश करें।
- विकासशील देशों को न्यूनतम ब्याज शर्तों पर ऋण दिलाए जाएँ और उनके पुनर्भुगतान की शर्ते भी अत्यधिक लचीली रखी जाएँ।
प्रश्न 10.
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएँ-
- भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति है।
- भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक स्वतन्त्र नीति है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थिरता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है।
- भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है।
- भारत की गुटनिरपेक्ष नीति नव-स्वतन्त्र देशों के गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है।
- भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अल्पविकसित देशों के आपसी सहयोग तथा आर्थिक विकास पर बल देती है।
प्रश्न 11.
भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति के अपनाए जाने के कारण भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति के अपनाए जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
- राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई ताकि वह स्वतन्त्र रूप से ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिनसे उसका हित सधता हो; न कि महाशक्तियों और खेमे के देशों का।
- दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेने हेतु-भारत ने दोनों महाशक्तियों से सम्बन्ध व मित्रता स्थापित करते हुए दोनों से सहयोग लेने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी।
- स्वतन्त्र नीति-निर्धारण हेतु-भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि भारत स्वतन्त्र नीति का निर्धारण कर सके।
- अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
शीतयुद्ध का क्या अर्थ है?
उत्तर:
शीतयुद्ध का अर्थ-अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित वादविवादों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, कूटनीतिक चालों तथा सैन्य शक्ति के प्रसार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को ‘शीतयुद्ध’ कहा जाता है।
प्रश्न 2.
अपरोध (रोक और सन्तुलन) का तर्क किसे कहा गया?
उत्तर:
अपरोध का तर्क-यदि कोई शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएँगे। इसे ‘अपरोध का तर्क’ कहा गया।
प्रश्न 3.
शीतयुद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था? . उत्तर शीतयुद्ध शुरू होने का मूल कारण-परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल सम्भावनाएँ थीं। इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण सरल कार्य न था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बच जाएँगे। यही कारण था कि तीसरा विश्वयुद्ध न होकर शीतयुद्ध की स्थिति बनी।
प्रश्न 4.
शीतयुद्ध के दायरे से आपका क्या अभिप्राय है? कोई एक उदाहरण भी दीजिए।
उत्तर:
शीतयुद्ध का दायरा-शीतयुद्ध के दायरे का अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ विरोधी गुटों में विभक्त देशों के मध्य संकट के अवसर आए, युद्ध हुए अथवा इनके होने की प्रबल सम्भावनाएँ उत्पन्न हुईं। कोरिया, वियतनाम तथा अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई परन्तु विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ भी बनीं जब दोनों महाशक्तियों के मध्य राजनीतिक वार्ताएँ नहीं हुईं तथा इसने दोनों के बीच की गलतफहमियाँ बढ़ाई।
प्रश्न 5.
शीतयुद्ध के किन्हीं दो सैनिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
शीतयुद्ध के दो सैनिक लक्षण निम्नलिखित हैं-
- नाटो, सिएटो, सेन्टो तथा वारसा पैक्ट इत्यादि सैन्य गठबन्धनों का निर्माण करना तथा इनमें अधिकाधिक देशों को सम्मिलित करना।
- शस्त्रीकरण करना तथा अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें निर्मित करके उन्हें युद्ध के महत्त्व के बिन्दुओं पर स्थापित करना।
प्रश्न 6.
छोटे देशों ने शीतयुद्ध के युग की मैत्री सन्धियों में महाशक्तियों के साथ अपने आपको क्यों जोड़ा? कोई दो कारण बताइए।
उत्तर:
छोटे देशों ने स्वयं को निम्नलिखित कारणों से महाशक्तियों के साथ जोड़ा था-
- छोटे देश असुरक्षा की भावना से ग्रसित थे। वे स्वयं को बड़ी शक्तियों से जोड़कर स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे।
- कुछ देशों की सोच थी कि यदि वे महाशक्तियों के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें अपनी सुरक्षा हेतु अधिक सैन्य व्यय नहीं करना होगा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता बिना किसी देरी के मिलेगी।
प्रश्न 7.
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के कोई दो लक्षण बताइए।
उत्तर:
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के दो लक्षण निम्नलिखित हैं-
- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश गुटीय राजनीति से दूर रहते हुए अपनी एक स्वतन्त्र विदेश नीति रखते हैं।
- विश्व में महायुद्ध जैसे किसी भी बड़े खतरे पर प्रभावी अंकुश लगाने में गुटनिरपेक्षता की नीति कारगर सिद्ध होती है। इसके द्वारा अनेक युद्धों का समाधान किया जा चुका है।

प्रश्न 8.
गुटनिरपेक्षता की किन्हीं दो नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
गुटनिरपेक्षता की दो नवीन प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-
- वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नव-उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में संलग्न है।
- धीरे-धीरे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने एक राजनीतिक आन्दोलन से आर्थिक आन्दोलन का स्वरूप धारण कर लिया है।
प्रश्न 9.
बाण्डुंग सम्मेलन क्या है? इसके कोई दो परिणाम लिखिए।
उत्तर:
बाण्डंग सम्मेलन-सन् 1955 में इण्डोनेशिया के एक शहर बाण्डंग में एफ्रो-एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम ‘बाण्डुंग सम्मेलन’ के नाम से जानते हैं।
बाण्डुंग सम्मेलन के दो परिणाम निम्नलिखित हैं-
- अफ्रीका तथा एशिया के नव-स्वतन्त्र देशों के साथ भारत के निरन्तर बढ़ते हुए सम्पर्कों का यह चरम बिन्दु था।
- बाण्डुंग सम्मेलन के दौरान ही गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की आधारशिला रखी गई थी।
प्रश्न 10.
शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच हुई किन्हींचार मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
शीतयुद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच निम्नलिखित मुठभेड़ हुईं –
- सन् 1950-53 का कोरिया युद्ध तथा कोरिया का दो भागों में विभक्त होना।
- सन् 1959 का फ्रांस एवं वियतनाम का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई।
- बर्लिन की दीवार का निर्माण।
- क्यूबा मिसाइल संकट (1962)।
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था-
(a) 1967
(b) 1971
(c) 1975
(d) 1962
उत्तर:
(d) 1962
प्रश्न 2.
बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई-
(a) 1961 में
(b) 1962 में
(c) 1960 में
(d) 1971 में।
उत्तर:
(a) 1961 में।
प्रश्न 3.
वारसा सन्धि कब हुई-
(a) 1965 में
(b) 1955 में
(c) 1957 में
(d) 1954 में।
उत्तर:
(b) 1955 में।
प्रश्न 4.
गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था-
(a) नई दिल्ली में
(b) हरारे में
(c) काहिरा में
(d) बेलग्रेड में।
उत्तर:
(d) बेलग्रेड में।

प्रश्न 5.
प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था-
(a) 1945 में
(b) 1949 में
(c) 1961 में
(d) 1955 में।
उत्तर:
(c) 1961 में।
![]()
![]()
![]()
![]()