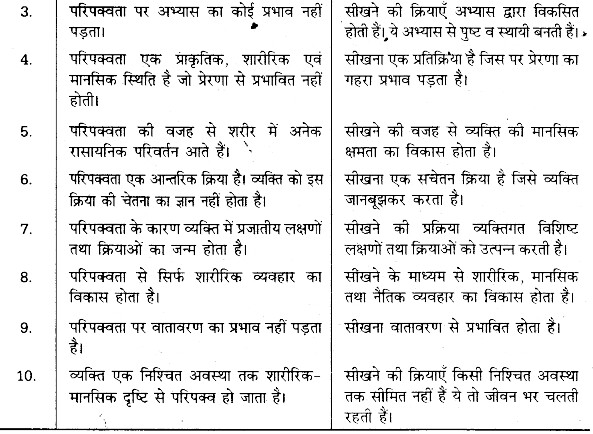UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य are part of UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य.
| Board |
UP Board |
| Textbook |
NCERT |
| Class |
Class 12 |
| Subject |
Samanya Hindi |
| Chapter Name |
सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य |
| Category |
UP Board Solutions |
UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य
सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्ध
भारतीय समाज में नारी का स्थान [2009]
सम्बद्ध शीर्षक
- भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति [2012]
- आधुनिक भारत में नारी का स्थान
- आधुनिक नारी का स्थान
- स्वातन्त्र्योत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति
- भारतीय नारी : आज और कल [2013]
- नारी सम्मान : भारतीय संस्कृति की पहचान [2014]
- नारी-चिन्तन का बदलता स्वरूप (2015)
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- भारतीय नारी का अतीत,
- मध्यकाल में भारतीय नारी,
- आधुनिक युग में नारी,
- पाश्चात्य प्रभाव एवं जीवन-शैली में परिवर्तन,
- उपसंहार
प्रस्तावना-गृहस्थीरूपी रथ के दो पहिये हैं—नर और नारी। इन दोनों के सहयोग से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। इसमें भी नारी का घर के अन्दर और पुरुष का घर के बाहर विशेष महत्त्व है। फलतः प्राचीन काल में ऋषियों ने नारी को अतीव आदर की दृष्टि से देखा। नारी पुरुष की सहधर्मिणी तो है ही, वह मित्र के सदृश परामर्शदात्री, सचिव के सदृश सहायिका, माता के सदृश उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली और सेविका के सदृश उसकी अनवरत सेवा करने वाली है। इसी कारण मनु ने कहा है, ”यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” अर्थात् जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर भी भारत में नारी की स्थिति एक समान न रहकर बड़े उतार-चढ़ावों से गुजरी है, जिसका विश्लेषण वर्तमान भारतीय समाज को समुचित दिशा देने के लिए आवश्यक है।
भारतीय नारी का अतीत-वेदों और उपनिषदों के काल में नारी को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वह पुरुष के समान विद्यार्जन कर विद्वत्सभाओं में शास्त्रार्थ करती थी। महाराजा जनक की सभा में हुआ याज्ञवल्क्य-गार्गी शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी भारती अपने काल की अत्यधिक विख्यात विदुषी थीं, जिन्होंने अपने दिग्गज विद्वान् पति की पराजय के बाद स्वयं आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। यही नहीं, स्त्रियाँ युद्ध-भूमि में भी जाती थीं। इसके लिए कैकेयी का उदाहरण प्रसिद्ध है। उस काल में नारी को अविवाहित रहने या स्वेच्छा से विवाह करने का पूरा अधिकार था। कन्याओं का विवाह उनके पूर्ण यौवनसम्पन्न होने पर उनकी इच्छा व पसन्द के अनुसार ही होता था, जिससे वे अपने भले-बुरे का निर्णय स्वयं कर सकें।
मध्यकाल में भारतीय नारी-मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गयी; क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण से हिन्दू-समाज का मूल ढाँचा चरमरा गया और वे परतन्त्र होकर मुसलमान शासकों का अनुकरण करने लगे। मुसलमानों के लिए स्त्री मात्र भोग-विलास और वासना-तृप्ति की वस्तु थी। फलत: लड़कियों को विद्यालय में भेजकर पढ़ाना सम्भव न रहा। हिन्दुओं में बाल-विवाह का प्रचलन हुआ, जिससे लड़की छोटी आयु में ही ब्याही जाकर अपने घर चली जाए। परदा-प्रथा का प्रचलन हुआ और नारी घर में ही बन्द कर दी गयी। युद्ध में पतियों के पराजित होने पर यवनों के हाथ न पड़ने के लिए नारियों ने अग्नि का आलिंगन करना शुरू किया, जिससे सती–प्रथा का प्रचलन हुआ। इस प्रकार नारियों की स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी और वे मात्र दासी या भोग्या बनकर रह गयीं। नारी की इसी असहायावस्था का चित्रण गुप्त जी ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है-
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ।।
आधुनिक युग में नारी-आधुनिक युग में अंग्रेजों के सम्पर्क से भारतीयों में नारी-स्वातन्त्र्य की चेतना जागी। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सामाजिक आन्दोलन का भी सूत्रपात हुआ। राजा राममोहन राय और महर्षि दयानन्द जी ने समाज-सुधार की दिशा में बड़ा काम किया। सती–प्रथा कानून द्वारा बन्द करायी गयी और बाल-विवाह पर रोक लगी। आगे चलकर महात्मा गाँधी ने भी स्त्री-सुधार की दिशा में बहुत काम किया। नारी की दीन-हीन दशा के विरुद्ध पन्त का कवि हृदय आक्रोश प्रकट कर उठता है-
मुक्त करो नारी को मानव
चिरबन्दिनी नारी को।
आज नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें उनकी योग्यतानुसार आर्थिक स्वतन्त्रता भी मिली हुई है। स्वतन्त्र भारत में आज नारी किसी भी पद अथवा स्थान को प्राप्त करने से वंचित नहीं। धनोपार्जन के लिए वह आजीविका का कोई भी साधन अपनाने के लिए स्वतन्त्र है। फलतः स्त्रियाँ अध्यापिका, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील, जज, प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, अपितु पुलिस में नीचे से ऊपर तक विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। स्त्रियों ने आज उस रूढ़ धारणा को तोड़ दिया है कि कुछ सेवाएँ पूर्णत: पुरुषोचित होने से स्त्रियों के बूते की नहीं। आज नारियाँ विदेशों में राजदूत, प्रदेशों की गवर्नर, विधायिकाएँ या संसद सदस्याएँ, प्रदेश अथवा केन्द्र में मन्त्री आदि सभी कुछ हैं। भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमन्त्रित्व तक एक नारी कर गयी, यह देख चकित रह जाना पड़ता है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कर सबको दाँतों तले अँगुली दबवा दी। इतना ही नहीं, नारी को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाने के लिए उसे कानून द्वारा पिता एवं पति की सम्पत्ति में भी भाग प्रदान किया गया है।
आज स्त्रियों को हर प्रकार की उच्चतम शिक्षा की सुविधा प्राप्त है। बाल-मनोविज्ञान, पाकशास्त्र, गृह-शिल्प, घरेलू चिकित्सा, शरीर-विज्ञान, गृह-परिचर्या आदि के अतिरिक्त विभिन्न ललित कलाओं; जैसे—संगीत, नृत्य, चित्रकला, छायांकन आदि में विशेष दक्षता प्राप्त करने के साथ-साथ वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों में भी वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
स्वयं स्त्रियों में भी अब सामाजिक चेतना जाग उठी है। प्रबुद्ध नारियाँ अपनी दुर्दशा के प्रति सचेत हैं। और उसके सुधार में दत्तचित्त भी। अनेक नारियाँ समाज-सेविकाओं के रूप में कार्यरत हैं। आशा है कि वे भारत की वर्तमान समस्याओं; जैसे-भुखमरी, बेकारी, महँगाई, दहेज-प्रथा आदि के सुलझाने में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
पाश्चात्य प्रभाव एवं जीवन-शैली में परिवर्तन–किन्तु वर्तमान में एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति भी नारियों में बढ़ती दीख पड़ती है, जो पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता का प्रभाव है। अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप अधिक शिक्षित नारियाँ तेजी से भोगवाद की ओर अग्रसर हो रही हैं। वे फैशन और आडम्बर को ही जीवन का सार समझकर सादगी से विमुख होती जा रही हैं और पैसा कमाने की होड़ में अनैतिकता की ओर उन्मुख हो रही हैं। यही बहुत ही कुत्सित प्रवृत्ति है, जो उन्हें पुन: मध्यकालीन-हीनावस्था में धकेल देगी। इसी बात को लक्ष्य कर कवि पन्त नारी को चेतावनी देते हुए कहते हैं-
तुम सब कुछ हो फूल, लहर, विहगी, तितली, मार्जारी,
आधुनिके ! कुछ नहीं अगर हो, तो केवल तुम नारी ।
प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती प्रेमकुमारी’ दिवाकर’ को कथन है कि, “आधुनिक नारी ने नि:सन्देह बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर सब-कुछ पाकर भी उसके भीतर का परम्परा से चला आया हुआ कुसंस्कार नहीं बदल रहा है। वह चाहती है कि रंगीनियों से सज जाए और पुरुष उसे रंगीन खिलौना समझकर उससे खेले। वह अभी भी अपने-आपको रंग-बिरंगी तितली बनाये रखना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक उसकी यह आन्तरिक दुर्बलता दूर नहीं होगी, तब तक उसके मानस का नव-संस्कार न होगा। जब तक उसका भीतरी व्यक्तित्व न बदलेगा तब तक नारीत्व की पराधीनता एवं दासता के विष-वृक्ष की जड़ पर कुठाराघात न हो सकेगा।”
उपसंहार-नारी, नारी ही बनी रहकर सबकी श्रद्धा और सहयोग अर्जित कर सकती है, तितली बनकर वह स्वयं तो डूबेगी ही और समाज को भी डुबाएगी। भारतीय नारी पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से आने वाली यूरोपीय संस्कृति के व्यामोह में न फंसकर यदि अपनी भारतीयता बनाये रखे तो इससे उसका और समाज दोनों का हितसाधन होगा और वह उत्तरोत्तर प्रगति करती जाएगी। वर्तमान में कुरूप सामाजिक समस्याओं; जैसे-दहेज प्रथा, शारीरिक व मानसिक हिंसा की शिकार स्त्री को अत्यन्त सजग होने की आवश्यकता है। उसे भरपूर आत्मविश्वास एवं योग्यता अर्जित करनी होगी, तभी वह सशक्त व समर्थ व्यक्तित्व की स्वामिनी हो सकेगी अन्यथा उसकी प्राकृतिक कोमल स्वरूप-संरचना तथा अज्ञानता उसे समाज के शोषण का शिकार बनने पर विवश कर देगी। नारी के इसी कल्याणमय रूप को लक्ष्य कर कविवर प्रसाद ने उसके प्रति इन शब्दों में श्रद्धा-सुमन अर्पित किये-
नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत-नभ-पग-तल में,
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ।
भारतीय नारी की समस्याएँ
सम्बद्ध शीर्षक
- कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ
- आधुनिक समाज में नारी की समस्याएँ
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना : वैदिक काल में नारी,
- मध्यकाल में नारी,
- आधुनिक काल में नारी,
- संविधान द्वारा दिये गये अधिकार,
- कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ,
- कामकाज से इतर महिलाओं की समस्याएँ,
- उपसंहार
प्रस्तावना : वैदिक काल में नारी—भारत में महिलाओं का स्थान कुछ वर्षों पहले तक घर-परिवार की सीमाओं तक ही सीमित माना जाता रहा है। प्राचीन भारत में नारी के पूर्ण स्वतन्त्र तथा सभी प्रकार के दबावों से पूर्ण मुक्त रहने के विवरण मिलते हैं। उस समय वे अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त किया करती थीं; क्योंकि तब शिक्षा प्रणाली आश्रम-व्यवस्था पर आधारित थी। इस कारण नारियाँ भी उन आश्रमों में पुरुषों के समान रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करती थीं। गार्गी, मैत्रेयी, अरुन्धती जैसी महिलाओं के विवरण भी मिलते हैं कि वे मन्त्र-द्रष्टा थीं। अपने पतियों के साथ आश्रमों में रहकर वहाँ की सम्पूर्ण व्यवस्था की, वहाँ रहने वाले अन्य स्त्री-पुरुष व विद्यार्थियों, यहाँ तक कि आश्रमवासी पशु-पक्षियों तक की वे देखभाल किया करती थीं। महर्षि वाल्मीकि और कण्व के आश्रमों में भी नारियों के निवास के विवरण मिलते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल में नारी सुरक्षित तो होती ही थी, प्रत्येक प्रकार से स्वतन्त्र भी हुआ करती थी। फिर भी ऐसे विवरण कहीं नहीं मिलते कि घर-गृहस्थी चलाने के लिए उसे कहीं काम करके धनोपार्जन भी करना पड़ता था। गृहस्वामिनी एवं माँ के रूप में उसे पिता एवं आचार्य से भी उच्च स्थान प्राप्त था। महाभारत में उल्लेख भी है कि “गुरुणां चैव सर्वेषां माता परमं को गुरुः।”
मध्यकाल में नारी–इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्यकाल में आकर नारी पूर्णरूपेण घरपरिवार की चारदीवारी में बन्द होकर रह गयी थी। यह काल नारियों के लिए अवनति का काल था। भोग-विलास की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण नारी के शारीरिक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। मध्यकालीन कुरीतियों में सती–प्रथा, बाल-विवाह और विधवाओं को हेय दृष्टि से देखना प्रमुख थीं । इस काल के सन्तों एवं सिद्ध कवियों ने भी नारी के प्रति अत्यन्त कटु दृष्टिकोण अपनाया-
नारी तो हम भी करी, जाना नहीं बिचार।
जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥
नारी की झाँई परत, अंधा होत भुजंग।।
कबिरा तिन की कौन गति, जेनित नारी के संग ।। (कबीरदास)
आधुनिक काल में नारी–अंग्रेजों के आगमन के बाद, कुछ उनके और कुछ उनकी चलाई शिक्षादीक्षा के, कुछ यहाँ चलने वाले अनेक प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों के प्रभाव से भारतीय नारी को घर-परिवार से बाहर कदम रखने का अवसर मिला। इस काल में महान् समाज-सुधारक राजा राममोहन राय ने सती–प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षा आदि पर जोर दिया। महात्मा गाँधी ने अछूतोद्धार की भाँति नारी मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। समाज-सुधारकों के सामूहिक प्रयास, देश में सामाजिक और राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव तथा प्रगतिशील विचारधारा ने नारी दासता की बेड़ियों को काटा और वह मुक्ति की ओर अग्रसर हुई। आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। वह राजनीतिज्ञ, राजनयिक, विधिवेत्ता, न्यायाधीश, प्रशासक, कवि, चिकित्सकै आदि के रूप में समाज को अपना योगदान दे रही है।
संविधान द्वारा दिये गये अधिकार-स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् लागू भारतीय संविधान में (अनुच्छेद 14 और 15) पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण समानता की गारण्टी दी गयी तथा लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करने की बात कही गयी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में लड़की को लड़के के समान सह-उत्तराधिकारी बना दिया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 ने विशेष आधारों पर विवाह के सम्बन्ध को समाप्त करने की अनुमति दी। दहेज को अवैध घोषित किया गया तथा इसके लिए सजा की व्यवस्था की गयी। दहेज की विकरालता को देखते हुए सन् 1961 में एक दहेज विरोधी कानून बनाया गया।
बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नारी ने लगभग प्रत्येक आन्दोलन में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर योगदान दिया है तथा समाज की प्रत्येक समस्या के विरुद्ध अपनी आवाज उठायी है। शोषण की घटनाओं के विरुद्ध तो उसने शक्तिशाली प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। यह इस बात का संकेत है कि महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता आयी है। नारियों को विभिन्न स्तरों पर आरक्षण देने की बातें हो रही हैं, परन्तु संविधान में यह व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है।
कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ-अभाव और महँगाई से दो-चार होने के लिए महिलाओं को कुछ मात्रा में स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले और अधिकतर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई तरह के काम-काज का भी सहारा लेना पड़ा। पुरुषों एवं महिलाओं का एक वर्ग यह समझता है कि कामकाजी नारी की समस्त समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। नौकरी मिलते ही नारी नारीत्व के अभिशापों से मुक्त हो जाती है, परन्तु वस्तुस्थिति सर्वथा भिन्न है, यथा–
(1) नारी कामकाजी महिला बनने का निर्णय लेने में स्वतन्त्र नहीं होती है। विवाह के पहले माता-पिता और बाद में ससुरालीजनों की इच्छा पर निर्भर रहता है कि वह कामकाजी बनी रहे अथवा नहीं।
(2) कामकाजी होने पर भी महिला आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं बन पाती है। उसको अपनी कमाई का हिसाब घरवालों को देना पड़ता है। प्रायः यह भी देखने में आता है कि ससुराल वाले विवाह के पूर्व की जाने वाली उसकी कमाई का भी हिसाब माँगते हैं।
(3) दोहरी जिम्मेदारी-कामकाजी महिलाओं को नौकरी से लौटकर घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। अत: एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सँभालकर भी कामकाजी महिलाएँ अपनी पूर्व जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पायी हैं।।
(4) बच्चों की परवरिश-कामकाजी महिलाओं के पास बच्चों को देने के लिए समय का अभाव होता है। फलतः उनके बच्चे संस्कारित नहीं हो पाते और उनका भविष्य बिगड़ जाने की सम्भावना रहती है।
(5) समाज में बदनामी-आधुनिक युग में भी स्त्रियों का नौकरी करना उचित नहीं माना जाता। बहू को नौकरी नहीं करने देने के लिए सास-ससुर, देवर-ज्येष्ठ और पति तक भी तनकर खड़े हो जाते हैं।
(6) परिजनों का शक-नौकरी-पेशा करने वाली महिलाएँ चरित्र के प्रति सन्देह की समस्या से कभी नहीं उबर पाती हैं। कार्यालय में किसी भी कारण से थोड़ी भी देर हो जाए तो परिजनों, विशेषकर पति की शक की निगाहें उसे अन्दर तक बेध डालती हैं। यह समस्या उस वक्त और भी बढ़ जाती है, जब महिला कोई स्टेनो या सेक्रेटरी हो।
(7) यौन शुचिता–आज भी स्त्री की सबसे बड़ी समस्या उसकी यौन शुचिता है। ऑफिस में किसी भी मुस्कराहट या स्पर्श से भी वह दूषित हो जाती है। यौन शुचिता का यह परिवेश नारी को खुलकर कार्य करने से रोकता है तथा उसकी प्रतिभा को कुण्ठित करता है।
(8) यौन-शोषण-सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाएँ पूर्ण तो नहीं, किन्तु अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के भी यौन-शोषण होते हैं, किन्तु निजी संस्थानों में अथवा मजदूरी करने वाली महिलाओं की दशा तो अत्यधिक दारुण है।
(9) वरीयता का मापदण्ड योग्यता नहीं–प्राइवेट संस्थानों के रोजगार विज्ञापनों में स्मार्ट, सुन्दर व आधुनिक महिलाओं की वरीयता यह प्रश्न खड़ा करती है कि कार्यक्षमता के आधार पर आगे बढ़ने वाले निजी संस्थानों का काम क्या स्मार्ट, सुन्दर व आधुनिक महिलाएँ ही सँभाल सकती हैं ? योग्यता कोई मापदण्ड नहीं? यह भी एक बीमार मानसिकता की परिचायक है।
(10) परिधान-कामकाजी महिलाओं के लिए परिधान (ड्रेस) बहुत बड़ी समस्या रहती है। वह जरा-सी भी सज-सँवर करके चले तो उस पर फब्तियाँ कसी जाती हैं, उसको तितली अथवा फैशन परेड की नारी कहा जाता है।
(11) पुरुषों की अपेक्षा सौतेला व्यवहार-महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। तथा पुरुषों की तुलना में इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। पहले विमान परिचारिकाओं के गर्भवती होते ही उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाता था। लम्बे संघर्ष के उपरान्त अब विमान परिचारिकाओं ने माँ बनने का अधिकार पाया है।
(12) बाहरी दौरे-कार्य के लिए अपने गृह जिले के बाहर जाना भी कामकाजी महिलाओं की एक प्रमुख समस्या है। घर की जिम्मेदारी, शील व गरिमा की चिन्ता, पति व बच्चों से आत्मीयता आदि उसे दौरे पर जाने से रोक देते हैं।
(13) रात्रि ड्यूटी-कामकाजी महिलाओं के लिए रात्रि ड्यूटी करना बहुत कठिन होता है। लोगों की शक की निगाहें मुसीबत कर देती हैं। अस्पतालों में रात्रि की पारी में काम करने वाली नर्से, बड़े होटलों में काम करने वाली महिलाएँ अपनी ड्यूटी सुरक्षित निकालकर सुकून का अनुभव करती हैं।
(14) नारी की नौकरी यदि पति की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है तो उसको पति की हीन भावना का भी शिकार होना पड़ता है।
(15) नौकरी करते हुए पति-पत्नी एक ही स्थान पर कार्यरत रहें, तब तो कुछ ठीक है, अन्यथा उनका दाम्पत्य तथा गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाते हैं, वैसे भी कामकाजी महिलाओं की गृहस्थी अव्यवस्थित तो हो ही जाती है।
(16) कुछ कामकाजी महिलाओं के लिए तो नौकरी अभिशाप बन जाती है। ऐसा प्रायः उन महिलाओं के साथ होता है, जिनके पतियों की आमदनी कम होती है, अथवा पति शराबी व कुमार्गी होते हैं। ऐसे पति अपनी पत्नी की आमदनी को भी उड़ाने के लिए पत्नी को भाँति-भाँति से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित करते हैं।
कामकाज से इतर महिलाओं की समस्याएँ-सुधारों की गर्जना तथा संवैधानिक प्रयास नारी की मौलिक समस्याओं को सुलझा नहीं सके हैं। संविधान ने नारी को मताधिकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दे दिया है, परन्तु समाज की दृष्टि में नारी को आज भी पुरुष की अंकशायिनी और दासी ही माना जाता है। हम आज भी अनेकानेक नारियों के उत्पीड़न, आत्मदाह तथा उनकी हत्या के समाचार सुनते रहते हैं। इनमें नौकरी करने वाली यानी कामकाजी महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। आज भी दहेज का दानव नारी के जीवन को त्रस्त किये हुए है। विधवा-विवाह के नाम पर आज भी लोग नाक-भौंह सिकोड़ते हैं। नारी की उन्नति के नाम पर हम कितनी भी बातें करें, परन्तु नारी आज भी उपेक्षित है। वह घर-परिवार में एक सामान्य नारी से अधिक कुछ नहीं है। आज भी गर्भ में बच्ची (लड़की) को मार दिया जाता है तथा प्रसूति के समय दूषित प्रकृति का शिकार होना पड़ता है। अपनी रक्षा के लिए मुस्तैद नारी पर लोग तरह-तरह की फब्तियाँ कसते हैं।
उपसंहार-महिला हो या पुरुष, काम करना किसी के लिए भी अनुचित या बुरा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता, घर-परिवार और समूचे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी बनायी जाएँ, ऐसे उचित वातावरण का निर्माण किया जाए कि कामकाजी महिला भी पुरुष के समान व्यवहार और व्यवस्था पा सके। नारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए फैमिली कोर्ट बनाये जाने चाहिए और उनके प्रति किये जाने वाले आपराधिक मामलों में तकनीकी नहीं, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दहेज, बलात्कार, अपहरण आज की नारी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। नारियों के समर्थन में किये जाने वाले हमारे आन्दोलन पश्चिम के अन्धानुकरण को लेकर नहीं होने चाहिए। उनको भारतीय गृहिणी के आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए। पाश्चात्य चिन्तन के अन्धानुकरण से इस देश की नारियों को भी जल्दी-जल्दी तलाक, अवैध शिशु-जन्म आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जब तक नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक नारी का जीवन त्रस्त ही बना रहेगा। भारतीय नारी की मुक्ति के लिए सांस्कृतिक आन्दोलन की आवश्यकता है, संविधान और कानून तो उसमें सिर्फ मुददगार हो सकते हैं।
महिला सशक्तीकरण (2017)
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- सशक्तीकरण का अर्थ,
- महिला सशक्तीकरण अभियान,
- महिला सशक्तीकरण अभियान के उद्देश्य- (क) महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को समाप्त करना, (ख) लिंगानुपात को सन्तुलित करना, (ग) लिंग-आधारित आर्थिक असमानता को समाप्त करना, (घ) बाल-विवाह पर रोक लगाना, (ङ) लड़कियों को शिक्षित करना, (च) सीमान्त तथा शोषित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाना, (छ) महिलाओं की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना,
- महिलाओं की संवैधानिक स्थिति,
- महिला सशक्तीकरण अधिनियम,
- महिला सशक्तीकरण और समाज,
- उपसंहार।
प्रस्तावना-भारतीय समाज में नारियों को शक्तिस्वरूपा मानते हुए उनकी पूजा होती रही है। प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ भारतीय नारियों की गौरवगाथा से भरे हुए हैं।‘मनुस्मृति’ में कहा गया है
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः
अर्थात् जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय समाज में नारियों की दशा और दिशा में काल परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता रहा है। किसी युग में नारी को पूजा गया तो किसी युग में उसके अपमान, उत्पीड़न और अत्याचार की सीमाएँ पार कर दी गईं। महिलाएँ समाज में अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का भी शिकार होती रहती हैं। भारतीय समाज का ताना-बाना ऐसा है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ पिता, पति या पुत्र पर ही आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। निर्णय लेने का अधिकार भी पुरुषों का ही होता है। उनके इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही महिला सशक्तीकरण की अवधारणा का जन्म हुआ, जिससे महिलाएं अपने जीवन से जुड़ी प्रत्येक निर्णय स्वयं ले सकें और परिवार तथा समाज में अच्छी प्रकार रह सकें। महिलाओं के वास्तविक अधिकारों के विषय में जानकारी देकर उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तीकरण है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कहा था- “लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जाग्रत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।”
सशक्तीकरण का अर्थ–सशक्तीकरण अर्थ है-शक्तिशाली बनाना। वर्तमान में महिला सशक्तीकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं के सन्दर्भ में देखा जा रहा है। इसमें जागरूकता, अधिकारों को जानने, सहभागिता और निर्णय लेने के अधिकार जैसे घटक को सम्मिलित किया गया है। लीला मीहेनडल के अनुसार-“निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तीकरण में सहायक हैं।
महिला सशक्तीकरण अभियान–सरकार द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सन् 2001 ई० में महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की गई। इसके अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं के विधिक अधिकारों को सशक्त करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को दृढ़ बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे शासकीय प्रयासों में कुछ सामाजिक और संस्थानात्मक अवरोध सामने आए हैं। इन अवरोधों का उन्मूलनकर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से 8 मार्च, 2010 ई० को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण अभियान नामक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। भारत में सभी राज्यों एवं सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुँचाना है।
महिला सशक्तीकरण अभियान के उद्देश्य-महिला सशक्तीकरण अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
(क) महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को समाप्त करना-महिलाओं को सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा के अन्तर्गत अनेक प्रकार की प्रताड़नाएँ आती हैं; जैसे-मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न एवं दहेज-सम्बन्धी प्रताड़ना आदि। महिला सशक्तीकरण का दृष्टिकोण यह है कि महिलाएँ इन उत्पीड़नरूपी हिंसा व भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
(ख) लिंगानुपात को सन्तुलित करना—लैंगिक असमानता भारत का प्रमुख सामाजिक मुद्दा है, जिसमें महिलाएँ निरन्तर पिछड़ती जा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ हैं। इस असमानता को समाप्त करने के लिए महिला सशक्तीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है।
(ग) लिंग-आधारित आर्थिक असमानता को समाप्त करना-महिलाएँ किसी प्रकार भी पुरुषों से कम नहीं हैं। यदि वे वही कार्य करती हैं जो पुरुष करते हैं तो उन्हें पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जबकि समाज में ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समान काम, समान वेतन’ की व्यवस्था की गयी है। महिला सशक्तीकरण में इस आर्थिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
(घ) बाल-विवाह पर रोक लगाना-राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के अथक प्रयासों द्वारा बाल-विवाह निरोधक अधिनियम (1955) बना, परन्तु आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी के कारण बाल-विवाह का प्रचलन है। इस विवाह से अवयस्क माता और शिशु के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। महिला सशक्तीकरण द्वारा इस पर रोक लगाई जा रही है।
(ङ) लडकियों को शिक्षित करना--शिक्षा अज्ञानतारूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है। भारतीय समाज में लड़की को पराया धन मानकर उसी शिक्षा एवं अन्य सुख-सुविधाओं की उपेक्षा की जाती है, परन्तु आज महिला सशक्तीकरण आन्दोलन के कारण इस दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। आज लड़कियों के स्कूल में पंजीकरण एवं उनकी उपस्थिति में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार-“महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, स्वतन्त्र आय तथा सामाजिक परिस्थिति में सुधार ने परिवार में उनकी निर्णय क्षमता को बढ़ाया है और महिलाओं के समावेशन (सशक्तीकरण) के मार्ग को प्रशस्त किया है।”
(च) सीमान्त तथा शोषित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाना–महिला सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत सीमान्त महिलाओं (वेश्याओं) को वेश्यालयों से रिहा कराना, यौन शोषित एवं एड्स से पीड़ित, विधवाओं, बेसहाराओं, आतंकवाद की शिकार तथा विक्षिप्त महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, देखभाल, परामर्श, रोजगारपरक प्रशिक्षण, जागरूकता, पुनर्वास आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं और उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने को साहसपूर्ण एवं सराहनीय कदम उठाया जाता है। इस प्रयास से अनेक महिलाओं का जीवन सुधारा जा सका है।
(छ) महिलाओं की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना–स्वार्थी तत्त्वों द्वारा महिलाओं की खरीद-फरोख्त के अवैध व्यपार को रोकने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने से लेकर उनकी रिहाई, पुनर्वास, पुन:एकीकरण और पुनस्र्थापन का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में अनेक एन०जी०ओ० तथा हेल्पलाइनें महिला उन्नयन का कार्य कर रही हैं।
महिलाओं की संवैधानिक स्थिति-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39 (बी), 44 तथा अनुच्छेद 325 के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान की दृष्टि में स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है। समाज में जो भेद दृष्टिगोचर होते हैं, वह सब अशिक्षा, संकीर्णता और स्वार्थलिप्सा आदि के कारण ही समाज में विद्यमान हैं।
महिला सशक्तीकरण अधिनियम–संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कुछ अधिनियम पास किए गए हैं; जैसे–एक बराबर पारिश्रमिक ऐक्ट, दहेज रोक अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, मेडिकल टर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट, बाल-विवाह रोकथाम ऐक्ट, लिंग परीक्षण तकनीक (लड़का-लड़की जाँच पर रोक) ऐक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-शौषण रोकने तथा उन्हें सुरक्षा देने सम्बन्धी ऐक्ट आदि। इन अधिनियमों का सही उपयोग कर महिलाएँ अपना शोषण रोकने में समर्थ हो रही हैं।
महिला सुरक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1090 शक्ति-योजना का शुभारम्भ किया गया है। यह महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक बहुआयामी योजना है। इसके अन्तर्गत मोबाइल द्वारा मात्र एक बटन दबाते ही पुलिस नियन्त्रण कक्ष को सूचना मिल जाती है और संकटग्रस्त महिला की स्थिीत (स्थान की पहचान) की सही जानकारी पुलिस को हो जाती है, जिससे पुलिस उस महिला की तुरन्त सहायता करती है।
महिला सशक्तीकरण और समाज-भूमण्डलीकरण के इस दौर में स्त्री-पुरुष समानता की दुहाई के साथ-साथ अनेक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ, हेल्पलाइनें महिलाओं के सशक्तीकरण और उत्थान में जुटे हुए हैं; फिर भी समाज में महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं आया है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वयं महिलाओं में आज भी अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति कूट-कूटकर भरी है। निरक्षर अथवा अल्पशिक्षित महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, सैकड़ों पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी पुत्र-रत्न की प्राप्ति के लिए तन्त्र-मन, झाड़-फेंक और ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसी हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है। उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति अभी 2 या 3 प्रतिशत ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष एक करोड़ पच्चीस लाख लड़कियाँ जन्म लेती हैं, लेकिन तीस प्रतिशत लड़कियाँ 15 वर्ष से पूर्व ही मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। राजनीति में भी महिलाओं का प्रवेश हो गया है, संसद में उनकी संख्या भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया है। खेलों, फिल्मों, लेखन, पत्रकारिता तथा सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में भी महिलाओं ने नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं, परन्तु अभी भी समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल पाया है, जिसकी वह अधिकारी है।
उपसंहार-अन्त में कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई ईश्वर या मसीहा अवतरित नहीं होगा और न ही समाज द्वारा नारीवाद की परिभाषा गढ़ने से कोई बात बनेगी। यह तभी सम्भव होग जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे आएँ, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। सरकारें भी केवल महिला अधिकारों और कानूनों की संख्या में वृद्धि न करें, बल्कि व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकार और कानून बनाएँ, जिससे वास्तविक सशक्तीकरण की अवधारणा को साकार किया जा सके।
नारी स्वातंत्र्य : उच्छंखलता या प्रगतिशीलता
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- राष्ट्र की प्रगति में नारी की भूमिका,
- नारी स्वातंत्र्य के विरुद्ध घृणित षड्यंत्र,
- स्वतन्त्रता का दुरुपयोग,
- नारी के बढ़ते कदम,
- उपसंहार।
प्रस्तावना-आज की नारी स्वतंत्र है। सत्ता की कुर्सी हो अथवा खेल का मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रयोगशाला हो या कला-साहित्य का संसार, आज नारी के लिए प्रत्येक क्षेत्र का द्वार पूर्ण रूप से खुला है। भारत में उपनिवेशवादरूपी राक्षस से लड़ने के लिए उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से ही नारी की दशा में सुधार के प्रयास आरम्भ हो गए थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् तो संवैधानिक रूप से भी उन्हें स्वावलम्बी तथा सर्वाधिकारसम्पन्न बना दिया गया। समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर भी उनके स्वातंत्र्य तथा हितों की रक्षा की गई है। विश्व के कई अन्य राष्ट्रों में भी आज नारी को समुचित स्थान प्राप्त है। वस्तुतः ‘स्वतन्त्र और सबल प्रस्थितिवाली नारी’ ही 21वीं सदी को 20वीं सदी की सबसे बड़ी देन है।
किन्तु पिछले कुछ समय से यह विवाद का विषय बन गया है कि नारी स्वातंत्र्य प्रगतिशीलता का पोषक है अथवा उच्छंखलता का। हमारे समक्ष कई उदाहरण हैं कि महिलाओं ने अपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर विश्व के सामने विकास को ऊँचा कीर्तिमान प्रस्तुत किया। इसके विपरीत कई ऐसे प्रमाण भी हैं। कि स्त्रियों ने अपने स्वातंत्र्य अधिकारों का दुरुपयोग कर समाज में उच्छृखलता और संस्कारहीनता को बढ़ावा दिया। जहाँ एक ओर संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा और कल्पना चावला जैसी नारियों ने प्रगति की ऊँचाइयों को छुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ युवतियों ने मॉडलिंग के बहाने अपनी देह प्रदर्शन जैसे घृणित कार्य कर समाज के संस्कार को गर्त में गिराया है। वास्तव में नारी स्वातंत्र्य पर चल रहा यह विवाद गम्भीर रूप से विचारात्मक तथा विश्लेषणात्मक है।
राष्ट्र की प्रगति में नारी की भूमिका–इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब-तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। मैत्रेयी, गार्गी, आंडाल, विश्वपारा, केशा आदि विदुषी स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए आज भी पूजनीय हैं। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, अरुन्धती राय आदि स्त्रियों ने साहित्य तथा राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चेनम्मा, रानी दुर्गावती, माँ जीजाबाई, देवी अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, शिरिमाओ भण्डारनायके, इन्दिरा गांधी, आंग सान सू की और एंजेला मार्केल आदि स्त्रियाँ प्रगति के मार्ग पर संघर्ष और सुनेतृत्व की स्पष्ट मूर्तियों के रूप में स्थापित हुईं। कला के क्षेत्र में एम०एस० सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, देविका रानी, वैजन्तीमाला, सुधा चन्द्रन, सोनाल मानसिंह, मीरा नायर, सरोज खान और फराह खान आदि स्त्रियों का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों; जैसे—चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, बैंकिंग, प्रशासन आदि में भी स्त्रियाँ अपनी सक्रिय तथा विकासोन्मुखी भूमिका निभा रही हैं। इनमें से किसी ने भी उच्छृखलता का मार्ग नहीं अपनाया।
नारी स्वातंत्र्य के विरुद्ध घृणित षड्यंत्र–इन प्रगतिशील तथा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद नारियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपनी स्वतन्त्रता का गलत फायदा उठा रही हैं तथा समाज में अनुशासनहीनता फैला रही हैं, ऐसे आरोप कुछ तो सत्य होते हैं, किन्तु कुछ पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित। आज के युग में मध्यमवर्गीय परिवारों में कामकाजी महिलाओं का प्रचलन बढ़ गया है। ऐसी कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यालय तथा घर में सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। कार्यालयों में स्त्रियों को लिंग-भेद के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उच्चस्थ अधिकारी तथा साथी कर्मचारी उनके कार्य के नहीं, बल्कि सौन्दर्य के प्रशंसक होते हैं। असभ्य और असम्मानजनक टिप्पणियों का सामना करना आज महिलाओं के लिए दिनचर्या का अभिन्न अंग-सा बन गया है।
यदि स्त्रियाँ इस प्रकार की असभ्यता का विरोध करती हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है-यहाँ तक कि उन्हें सेवा से निष्कासन तक की धमकी दी जाती है और यदि वे अपने उच्चस्थ अधिकारियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं तो उन्हें पुंश्चली (वेश्या) और उच्छंखल की संज्ञा मिल जाती है। वस्तुत: नारी की ऐसी उच्छृखंलता के पीछे पुरुष की ही घृणित मंशा छिपी होती है। बाहर की इन परिस्थितियों से जूझते हुए महिलाएँ जब घर लौटती हैं तो घर के सभी काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। इस घोर थकावट के बावजूद उनसे आशा की जाती है। कि वे सदा मुस्कराती रहें। ऐसे में यदि कभी उनके चेहरे पर तनाव या चिन्ता की कोई रेखा पड़ जाती है, तो उन्हें असभ्य और उच्छृखल घोषित कर दिया जाता है। वस्तुत: पुरुष का दम्भ यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि जो नारी कल तक उसकी दासी-स्वरूपा थी, वह आज उसकी सहचरी बन गई है। इसलिए नारी-स्वतंत्रता के विरुद्ध घृणित षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।
स्वतंत्रता का दुरुपयोग-कई ऐसे प्रमाण भी हैं कि स्त्रियों ने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर उच्छंखलता का ही परिचय दिया है। ‘रानी मेरी’ की उच्छंखलता (क्रूरता) ने ही उन्हें इतिहास में ‘खूनी मेरी के नाम से कुख्यात किया। इन्दिरा गांधी द्वारा अधिरोपित दो वर्षों का आपातकाल आज तक उनके सफल व्यक्तित्व एवं स्वर्णिम शासनकाल पर बदनुमा दाग है। आज फिल्मोद्योग की कई अभिनेत्रियाँ सोचती हैं कि अंग-प्रदर्शन द्वारा वे दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो सकती हैं और इसलिए वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा को लाँघकर अंग-प्रदर्शन करती हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में तो स्थिति और भी बदतर है। फिल्म तथा मॉडलिंग से सम्बन्धित अधिकतर कार्यक्रमों एवं पत्रिकाओं में इस तरह की उच्छंखलता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नारियों में ऐसी उच्छृखलता सामान्य घरों में भी पाई जाती है। मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियाँ ऊँचे सपने देखती हैं और उन्हें साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। कुछ वर्ष पहले मुम्बई की व्यस्त सड़क पर मात्र पन्द्रह सौ रुपये तथा थोड़ी-सी लोकप्रियता के लिए दो लड़कियों ने बिना किसी झिझक के अपने कपड़े उतार दिए। यह घटना वास्तव में नारी-स्वतंत्रता पर उपादेयता का एक बड़ा प्रश्नचिह्न है और उच्छृखलता की पराकाष्ठा भी।
स्त्रियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग वास्तव में दु:खद है। यह पुरुष-प्रधान समाज सदा से ही नारी-स्वतंत्रता का विरोधी रहा है। ऐसे में महिलाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग तथा उच्छृखलता का। प्रदर्शन पुरुषों को उनके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने के अवसर प्रदान करते हैं। महिलाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग उन्हें नष्ट कर देगी। ऊंचे सपने देखना कदापि गलत नहीं है, किन्तु उन्हें साकार करने के लिए निम्नस्तरीय व्यवहार सदा ही गलत है। ‘नारी’ ही सम्पूर्ण विश्व की जननी है। विश्व की संस्कृति, प्रगति आदि सब उसी के गर्भ से उत्पन्न होती हैं। अत: आज नारी को विश्व के समक्ष ऐसा प्रतिमान स्थापित करना है कि उसकी अनिवार्यता और अपरिहार्यता को समग्र रूप से स्वीकार किया जा सके।
नारी के बढ़ते कदम-स्वतंत्रता का सदुपयोग तथा दुरुपयोग व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझते हैं और इसका प्रयोग स्वार्थ-सिद्धि तथा निजी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु करते हैं और कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को अपना उत्तरदायित्व मानते हैं और इसका निर्वहन अपने समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए करते हैं। महिलाओं में भी ये दो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, किन्तु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अत्यन्त कम है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो प्रगति के मार्ग पर अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है।
शारीरिक एवं मानसिक कोमलता के कारण पहले महिलाओं को रक्षा-सम्बन्धी सेवाओं के उपयुक्त नहीं माना जाता था, किन्तु भारत की पहली महिला भारतीय आरक्षी सेवा अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा से इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया। आज देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा में महिलाएँ समान रूप से संलग्न हैं। नारी-समुदाय पर यह आरोप लगाया जाता था कि वे पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वप्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में भावना गर्ग और विजयलक्ष्मी बिदारी जैसी नारियों ने इतिहास रचकर पुरुष के इस दंभ को भी तोड़ा है। पुरुष-वर्चस्व वाले फिल्मोद्योग में सर्वप्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता देविका रानी थीं। सितम्बर, 2001 में आयोजित 58वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लायन पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्मात्री मीरा नायर की फिल्म ‘मानसून वेडिंग’ को मिला। भारत के लिए सम्मान की बात यह है कि मीरा नायर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। जुलाई, 2016 में भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार तीन महिला लड़ाकू पायलटों ( भावना कान्त, अवनी चतुर्वेदी व मोहना सिंह) को शामिल किया गया। इस प्रकार, नारी को जिस क्षेत्र में अवसर तथा स्वातंत्र्य मिला, उसने अपने उच्चश्रेणी के कर्त्तव्य से वहीं विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।
वस्तुत: किसी देश की अन्त:संरचना तथा प्रगति नारी-स्वातंत्र्य के समानुपाती होती है, अर्थात् जिस देश में नारी की सहभागिता जितनी अधिक है, वहाँ की अन्त:संरचना उतनी ही मजबूत तथा प्रगति-दर उतनी ही तीव्र है।
उपसंहार–भारतीय जीवन का आधार वेद एवं शास्त्र हैं। शास्त्रों में लिखी बातें ही हमारे लिए प्रामाणिक होती हैं। नारी की स्वतंत्रता को प्रगति का आवश्यक तत्त्व मानकर ही शास्त्रों में लिखा गया है-
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”
(नारी की पूजा का अर्थ है–नारी की स्वतंत्रता और उसको प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार देवता सम्पन्नता के सूचक हैं।) इस प्रकार शास्त्रों में भी स्पष्ट है कि जहाँ नारी स्वतंत्र है वहाँ सम्पन्नता निश्चित है। उच्छंखलता व्यक्तिगत दोष है जो किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है, इसे स्वतंत्रता का परिणाम नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ विकास स्वतंत्रता का ही परिणाममात्र है।
नारी एवं पुरुष राष्ट्र के आधार हैं। दोनों ही विकासरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। यदि किसी एक पहिये में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध होगा तो गाड़ी का आगे बढ़ पाना असम्भव होगा; अतः आवश्यक है कि पहिए आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हों।
वर्तमान समाज पर दूरदर्शन का प्रभाव [2009]
सम्बद्ध शीर्षक
- दूरदर्शन : एक वरदान अथवा अभिशाप
- मेरे जीवन पर दूरदर्शन का प्रभाव
- दूरदर्शन : गुण एवं दोष
- दूरदर्शन और भारतीय समाज [2009]
- दरदर्शन : लाभ-हानि
- दूरदर्शन और आधुनिक जीवन
- दूरदर्शन का शैक्षिक उपयोग [2013, 14]
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- दूरदर्शन का आविष्कार,
- विभिन्न क्षेत्रों में योगदान.
- दूरदर्शन से हानियाँ,
- उपसंहार।
प्रस्तावना-विज्ञान द्वारा मनुष्य को दिया गया एक सर्वाधिक आश्चर्यजनक उपहार दूरदर्शन है। आज व्यक्ति जीवन की आपाधापी से त्रस्त है। वह दिनभर अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसका कार्य शारीरिक हो या मानसिक। शाम को थककर चूर हो जाने पर वह अपनी थकावट और नियों से मुक्ति के लिए कुछ मनोरंजन चाहता है। दूरदर्शन मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। आज यह जनसामान्य के जीवन का केन्द्रीय अंग हो चला है। दूरदर्शन पर हम केवल कलाकारों की मधुर ध्वनि को ही नहीं सुन पाते वरन् उनके हाव-भाव और कार्यकलापों को भी प्रत्यक्ष देख पाते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही साधन हो, ऐसा भी नहीं है। यह जनशिक्षा का एक सशक्त माध्यम भी है। इससे जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति का ज्ञानवर्द्धन हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से व्यक्ति का उन सबसे साक्षात्कार हुआ है जिन तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव भी था। दूरदर्शन ने व्यक्ति में जनशिक्षा का प्रसार करके उसे समय के साथ चलने की चेतना दी है। यूरोपीय देशों के साथ भारत में भी दूरदर्शन इस ओर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह रेडियो, सिनेमा और समाचार-पत्रों से अधिक अच्छा और प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है।
दूरदर्शन का आविष्कार-दूरदर्शन का आविष्कार अधिक पुराना नहीं है। 25 जनवरी, सन् 1926 ई० में इंग्लैण्ड के एक इंजीनियर जॉन बेयर्ड ने इसको रॉयल इंस्टीट्यूट के सदस्यों के सामने पहली बार प्रदर्शित किया। उसने रेडियो-तरंगों की सहायता से कठपुतली के चेहरे का चित्र बगल वाले कमरे में बैठे वैज्ञानिकों के सम्मुख दिखाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। विज्ञान के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी। भारत में दूरदर्शन का पहला केन्द्र सन् 1959 ई० में नयी दिल्ली में चालू हुआ था। आज तो सारे देश में दूरदर्शन का प्रसार हो गया है और इसका प्रसारण क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कृत्रिम उपग्रहों ने तो दूरदर्शन के कार्यक्रमों को समस्त विश्व के लोगों के लिए और भी सुलभ बना दिया है।
विभिन्न क्षेत्रों में योगदान–दूरदर्शन अनेक दृष्टियों से हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दूरदर्शन के योगदान, महत्त्व एवं उपयोगिताओं का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।
(1) शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन से अनेक शैक्षिक सम्भावनाएँ हैं। वह कक्षा में प्रभावशाली ढंग से पाठ की पूर्ति कर सकता है। विविध विषयों में यह विद्यार्थी की रुचि विकसित कर सकता है। यह कक्षा में विविध घटनाओं, महान् व्यक्तियों तथा अन्य स्थानों के वातावरण को प्रस्तुत कर सकता है। दृश्य होने के कारण इसका प्रभाव दृढ़ होता है। इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं को दूरदर्शन पर प्रत्यक्ष देखकर चारित्रिक विकास होता है। देश-विदेश के अनेक स्थानों को देखकर भौगोलिक ज्ञान बढ़ता है। अनेक पर्वतों, समुद्रों और वनों के दृश्य देखने से प्राकृतिक छटा के साक्षात् दर्शन हो जाते हैं।
(2) वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तरिक्ष के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान की दृष्टि से भी दूरदर्शन का विशेष महत्त्व रहा है। चन्द्रमा, मंगल व शुक्र ग्रहों पर भेजे गये अन्तरिक्ष यानों में दूरदर्शन यन्त्रों का प्रयोग किया गया था, जिनसे उन्होंने वहाँ के बहुत सुन्दर और विश्वसनीय चित्र पृथ्वी पर भेजे। बड़े देशों द्वारा अरबों रुपयों की लागत से किये गये विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानों को प्रदर्शित करके दूरदर्शन ने विज्ञान का उच्चतर ज्ञान कराया है तथा सैद्धान्तिक वस्तुओं का स्पष्टीकरण किया है।
(3) तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में-तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दूरदर्शन बहुत शिक्षाप्रद रहा है। दूरदर्शन ने एक सफल और प्रभावशाली प्रशिक्षक की भूमिका निभायी है। यह अधिक प्रभावशाली और रोचक विधि से मशीनी प्रशिक्षण के विभिन्न पक्ष शिक्षार्थियों को समझा सकता है। साथ ही यह लोगों को औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के विभिन्न पहलू प्रत्यक्ष दिखाकर उनसे परिचित कराता है।
(4) कृषि के क्षेत्र में–भारत एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ की तीन-चौथाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ अधिकांश कृषक अशिक्षित हैं। वे कृषि उत्पादन में पुरानी तकनीक को ही अपनाने के कारण अपेक्षित उत्पादन नहीं कर पाते। दूरदर्शन पर कृषि-दर्शन आदि विविध कार्यक्रमों से भारतीय कृषकों में जागरूकता आयी है।।
(5) सामाजिक चेतना की दृष्टि से-सामाजिक चेतना की दृष्टि से तो दूरदर्शन निस्सन्देह उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और अनेक बुराइयों पर कटु प्रहार किया है। लोगों को ‘छोटा परिवार सुखी परिवार की ओर आकर्षित किया है। इसने बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, छुआछूत व साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनमत तैयार किया है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन बाल-कल्याण और नारी-जागरण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह दर्शकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों, यातायात के नियमों, अल्प बचत, जीवन बीमा तथा कानून और व्यवस्था के विषय में भी शिक्षित करता है।
(6) राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शन राजनीतिक दृष्टि से भी जनसामान्य को शिक्षित करता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक होने के नाते उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। तथा मताधिकार के प्रति रुचि जाग्रत करके उसमें राजनीतिक चेतना लाता है। आजकल दूरदर्शन पर आयकर, दीवानी और फौजदारी मामलों से सम्बन्धित जानकारी भी दी जाती है, जिनके परिणामस्वरूप व्यक्ति का इस ओर ज्ञानवर्द्धन हुआ है।
(7) स्वस्थ रुचि के विकास की दृष्टि से--कवि सम्मेलन, मुशायरों, साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, नये प्रकाशनों का परिचय देकर तथा साहित्यकारों से साक्षात्कार प्रस्तुत करके दूरदर्शन ने साहित्य के प्रति स्वस्थ रुचि का विकास किया है। इसी प्रकार बड़े-बड़े कलाकारों की कलाओं की कला को परिचय देकर कला के प्रति लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ायी है। यही नहीं, नये उभरते हुए साहित्यकारों, कलाकारों (चित्रकार, संगीतकार, फोटोग्राफर आदि) एवं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कारीगरों के कृतित्व का परिचय देकर न केवल उनको प्रोत्साहित किया है, वरन् उनकी वस्तुओं की बिक्री के लिए व्यापक क्षेत्र भी प्रस्तुत किया है। इससे विभिन्न कलाओं को जीवित रखने और विकसित होने में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला है।
इतना ही नहीं, दूरदर्शन अन्य अनेक दृष्टिकोणों से जनसाधारण को जागरूक और शिक्षित करता है, वह चाहे खेल का मैदान हो या व्यवसाय का क्षेत्र। दूरदर्शन खेलों के प्रति रुचि जाग्रत करके खेल और खिलाड़ी की सच्ची भावना पैदा करता है। दूरदर्शन के सीधे प्रसारण ने कुश्ती, तैराकी, बैडमिण्टन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज आदि को लोकप्रियता की बुलन्दियों पर पहुँचा दिया है। दूरदर्शन के इस सुदृढ़ प्रभाव को देखते हुए उद्योगपति और व्यवसायी अपने उत्पादन के प्रचार और प्रसार के लिए इसे प्रमुख माध्यम के रूप में अपना रहे हैं।
दूरदर्शन से हानियाँ-दूरदर्शन से होने वाले लाभों के साथ-साथ इससे होने वाली कुछ हानियाँ भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोमल आँखें घण्टों तक टी० वी० स्क्रीन पर केन्द्रित रहने से अपनी स्वाभाविक शोभा क्षीण कर लेती हैं। इससे निकलने वाली विशेष प्रकार की किरणों का प्रतिकूल प्रभाव नेत्रों के साथ-साथ त्वचा पर भी पड़ता है, जो कि कम दूरी से देखने पर और भी बढ़ जाता है। इसके अधिक प्रचलन के परिणामस्वरूप विशेष रूप से बच्चों एवं किशोर-किशोरियों की शारीरिक गतिविधियाँ एवं खेलकूद कम होने लगे हैं। इससे उनके शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस पर प्रसारित होते कार्यक्रमों को देखते रहकर हम अपने अधिक आवश्यक कार्यों को या तो भूल जाते हैं या उनका करना टाल देते हैं। समय की बरबादी करने के साथ-साथ हम आलसी और कामचोर भी हो जाते हैं तथा हमें अपने आवश्यक कार्यों के लिए भी समय का प्रायः अभाव ही बना रहता है।
केबल टी०वी० पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों ने तो अल्पवयस्क बुद्धि के किशोरों को वासना के तूफान में ढकेलने का कार्य किया है। इनसे न केवल हमारी युवा पीढ़ी पर विदेशी अप-संस्कृति का प्रभाव पड़ता है अपितु हमारे अबोध और नाबालिग बच्चे भी इसके दुष्प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। । साथ ही विज्ञापनों के सम्मोहन ने धन के महत्त्व को धर्म और चरित्र से कहीं ऊपर कर दिया है। हानिकारक वस्तुओं को भी धड़ल्ले से बेचने का कार्य व्यापारी वर्ग लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से खूब कर रहा है।
उपसंहार-इस प्रकार हम देखते हैं कि दूरदर्शन मनोरंजन के साथ-साथ जनशिक्षा का भी एक सशक्त माध्यम है। विभिन्न विषयों में शिक्षा के उद्देश्य के लिए इसका प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता है कि इसे केवल मनोरंजन का साधन ही न समझा जाए, वरन् यह जनशिक्षा एवं प्रचार का माध्यम भी बने। इस उद्देश्य के लिए इसके विविध कार्यक्रमों में अपेक्षित सुधार होने चाहिए। इसके माध्यम से तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। सरकार दूरदर्शन के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए देश के विभिन्न भागों में इसके प्रसारण-केन्द्रों की स्थापना कर रही है। दूरदर्शन से होने वाली हानियों के लिए एक तन्त्र एवं दर्शन जिम्मेदार है। इसके लिए दूरदर्शन के निर्देशकों, सरकार एवं सामान्यजन को संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे, जिससे दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दोषमुक्त बनाकर उन्हें वरदान के रूप में ग्रहण किया जा सके।
मानवता का आधार : परोपकार
सम्बद्ध शीर्षक
- परहित सरिस धरम नहिं भाई [2009,15]
- परोपकार
- वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे (2015)
- परोपकार का महत्त्व
- परपीड़ा सम नहिं अधमाई
प्रमुख विचार-बिन्दु–
- प्रस्तावना,
- परोपकार की महत्ता अर्थात् परोपकार मानवीय धर्म,
- प्रकृति और परोपकार,
- परोपकार : मानवता का परिचायक,
- परोपकार के विविध रूप,
- परोपकार : आत्म-उत्थान का मूल,
- उपसंहार।
प्रस्तावनापरहित सरिस धरम नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई” अर्थात् दूसरे की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट पहुँचाने से बढ़कर कोई नीच काम नहीं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ धर्म की सुन्दर परिभाषा प्रस्तुत करती हैं।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अत: समाज में एक-दूसरे का सहयोग किये बिना वह पूर्ण मानव नहीं बन सकता। कोई भी मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं है, किसी-न-किसी कार्य के लिए वह दूसरे पर आश्रित रहता ही है। हम दूध-दही के लिए पशुओं पर, फल-फूल तथा अन्नादि के लिए वृक्षों पर, जल के लिए बादल एवं नदियों पर आश्रित हैं। ये सभी बिना किसी स्वार्थ के हमें यही सन्देश प्रदान करते हैं।
परोपकार की महत्ता अर्थात् परोपकार मानवीय धर्म–महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर वध के लिए देवताओं द्वारा माँगने पर अपनी हड्डियों को प्रदान करते हुए मानवीय परोपकार का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनकी हड्डियों से निर्मित सर्वाधिक कठोर वज्र के निर्माण से ही देवता वृत्रासुर का वध कर सके। मानव द्वारा देवों की रक्षा करने के लिए त्याग-भावना द्वारा मानव देक्ताओं से भी महान् दिखाई देने लगता है। महाराज शिवि ने भी करुणा-भावना के वशीभूत एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट-काट कर कबूतर को खाने के लिए आये बाज को खिलाकर परोपकार के क्षेत्र में प्रतिमान उपस्थित किया। वास्तव में ये महान् पुरुष धन्य हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर व प्राणों की भी चिन्ता नहीं की। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने इनकी वन्दना करते हुए उचित ही कहा है
क्षुधार्त्त रन्तिदेव ने दिया करस्थ थाल भी,
तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी।
उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया,
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया ।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।
इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे हजारों क्रान्तिकारी देशभक्तों ने भी नयी पीढ़ी की स्वतन्त्रता एवं सुख-समृद्धि के लिए परोपकार भावना से अनुप्राणित होकर अपने माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं परिवार की तनिक भी चिन्ता न करते हुए अपने प्राणों को हँसते-हँसते देश की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। संसार में उन्हीं व्यक्तियों के नाम अमर होते हैं, जो दूसरों के लिए मरते और जीवित रहते हैं। सीता की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले गिद्धराज जटायु से श्रीराम कहते हैं, “तुमने अपने सत्कर्म से ही सद्गति का अधिकार पाया है, इसका श्रेय मुझे नहीं है”
परहित बस जिनके मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नहीं ॥
प्रकृति और परोपकार-प्रकृति में परोपकार का नियम अप्रतिहत गति से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। सूर्य बिना किसी जाति, देश, वर्ण के भेदभाव के समानता-असमानता की भावना से, बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के, समस्त संसार को अपने प्रकाश और उष्णता से जीवन प्रदान करते हैं। वायु सभी को प्राण प्रदान कर रही है। चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से सभी को रस एवं शीतलता प्रदान करता है। पृथ्वी रहने को स्थान देती है। मेघ वर्षा ऋतु में आकर फसलों को हरा-भरा कर देते हैं। वृक्ष तो फूल, फल, छाल, शाखाएँ, ऑक्सीजन, जल, पत्ते, लकड़ियाँ, छाया आदि सर्वस्व प्रदान कर मानव-जीवन को आनन्दित बना देते हैं। झरने, प्रपात और नदियाँ अपने अमृतमय जल से पिपासा शान्त करती हुई, विद्युत एवं तैरने के अवसर, नौकाविहार, जलचरों को जीवन प्रदान करती हुई परोपकार की देवी ही बनी हुई है। कहा भी गया है-
बृच्छ कबहुँ नहिं फल भखें, नदी न संचै नीर।
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर ॥
अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, वृक्ष, वायु आदि ऐसा किसी प्रतिफल प्राप्ति की भावना से नहीं करते हैं, वे केवल अपने जन्मजात स्वभाववश ही ऐसा करते हैं। तब क्या प्रकृति की ही एक देन, मनुष्य, का यह कर्तव्य नहीं है कि वह दूसरों के हित में अपने जीवन को कुछ समय ही लगा दे।
परोपकार : मानवता का परिचायक–परोपकार ही मानव को महामानव बनाने की सामर्थ्य रखता है। परोपकार से ही हमारी स्वार्थ-भावना नष्ट होती है और हम देवता के समान कहलाने लगते हैं
सूर्य, चन्द्र, बादल, सरिता, भू, पेड़, वायु कर पर उपकार।।
बन जाते हैं देवतुल्य क्या, देवों के सचमुच अवतार ॥
परोपकारी व्यक्ति समाज में सर्वत्र सम्मान प्राप्त कर देश एवं विश्व के पूज्य बन जाते हैं। परोपकार से ही मनुष्य विश्वबन्धुत्व की भावना की ओर अग्रसर होता है। जनकल्याण, प्राणिसेवा में निरत व्यक्ति परम आदरणीय हो जाता है-
जो पराये काम आता, धन्य है जग में वही।
द्रव्य ही को जोड़कर, कोई सुयश पाता नहीं ॥
परोपकार भाईचारे की भावना का विकास करता है। यही घृणा, द्वेष और स्वार्थ का नाशक है। सभी प्राणियों में अपने ईश्वर का अंश देखकर महापुरुष जगत् के कल्याण में प्रवृत्त हो जाते हैं। राजा रन्तिदेव अपना सर्वस्व दान में देकर अड़तालीस दिन तक भूखे रहे। उनचासवें दिन जब भोजन का प्रबन्ध हुआ तो एक याचक आ गया। उन्होंने वह भोजन याचक को खिलाकर सन्तोष धारण किया–
न त्वहं कामये स्वर्ग, न मोक्षं न पुनर्भवम् ।।
कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामार्तनाशनम् ॥
राजा रन्तिदेव ने स्वर्ग-मोक्ष न माँग कर मानव ही नहीं सभी प्राणियों की पीड़ा को दूर करने का वरदान माँगा। परोपकारियों को ही सज्जन एवं महापुरुष की पदवी प्रदान की जाती है, जो युगों तक प्रणम्य हो जाते हैं। अट्ठारह पुराणों के रचयिता व्यास जी ने भी परोपकार को पुण्य एवं परपीड़ा को पाप घोषित किया है-
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥
परोपकारी व्यक्ति नि:स्वार्थ परोपकार कर अलौकिक आनन्द का अनुभव करता है। किसी भूखे को भोजन देते समय, प्यासे को पानी पिलाते समय, ठण्ड से ठिठुरते को वस्त्र देते समय, रोगी की सेवा करते समय मानव को जो अपार आनन्द का अनुभव होता है, वह वर्णनातीत है। उस समय वह स्व-पर के भेद से ऊपर उठकर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति करता है। हमारी सांस्कृतिक परम्परा में यज्ञ परोपकार ही है, जिसके द्वारा ‘इदं न मम’ कहते हुए अग्नि में डाली गयी आहुति लाखों लोगों का कल्याण करती हुई विस्तृत हो जाती है।”
परोपकार के विविध रूप-नि:शुल्क लंगर, सदाव्रत, प्याऊ, विद्यालय, धर्मशाला, बगीचा, वृक्षारोपण, जलाशय, औषधालये, वस्त्र-वितरण, निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, गौशाला आदि की व्यवस्था करना परोपकार के ही विविध रूप हैं। परोपकार का क्षेत्र केवल मनुष्यों तक संकुचित नहीं है, उसमें पशु-पक्षी कीट-पतंग सभी सम्मिलित हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को प्रणाम करते हुए कहा है-
सियाराममय सब जग जानी। करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥
रहीम ने परोपकार की महिमा का बखान करते हुए लिखा है कि-
रहिमन यों सुख होत है, उपकारी के संग।
बाँटनवारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग॥
तात्पर्य यह है कि परोपकारी व्यक्ति को उसी प्रकार स्वतः ही आनन्द की उपलब्धि होती है, जिस प्रकार लगाने वाले के हाथों में मेंहदी का रंग स्वतः ही आ जाता है।
जहाँ पुल, सड़कें नहीं वहाँ पुल, सड़कों का निर्माण करना, कन्याओं के लिए रोजगार सीखने के नि:शुल्क प्रशिक्षण देना, उन्हें स्वावलम्बी बनाना, अकाल, भूकम्प, युद्धादि के अवसर पर अन्न, वस्त्र, निवास की व्यवस्था करना परोपकारी कार्यों की श्रेणी में आते हैं।
सामान्य व्यक्ति तर्क दे सकते हैं कि धन से सम्पन्न व्यक्ति ही परोपकार कर सकता है। विचार करने पर हम अनुभव करेंगे कि परोपकार के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपितु एक सेवाभावी मन की आवश्यकता होती है। हम राह भटके हुए को राह दिखा सकते हैं, सड़क के बीच में पड़े हुए केले के छिलके, कंकड़-पत्थर आदि को उठाकर एक किनारे पर फेंक सकते हैं। यह परोपकार ही तो है। हम किसी दुखिया के आँसू पोंछ सकें, किसी आहत व्यक्ति की आहों में साझीदार बन सकें, किसी के सिर पर रखे हुए बोझ को हलका कर सकें, किसी प्यासे को पानी पिला सकें आदि, तो हम परोपकार के आनन्द एवं पुण्य-फल का लाभ प्राप्त करने के सहज अधिकारी बन जाएँगे। निर्धन विद्यार्थियों को नि:शुल्क ट्यूशन उत्तम कोटि को परोपकार कहलाएगा।
परोपकार : आत्म-उत्थान का मूल-मनुष्य क्षुद्र से महान् और विरल से विराट् तभी बन सकता है, जब उसकी परोपकार-वृत्ति विस्तृत होती रहेगी। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने प्राणि-मात्र के हित को मानव-जीवन का लक्ष्य बताया है। यही व्यक्ति का समष्टिमय स्वरूप भी है। ज्यों-ज्यों आत्मा में उदारता बढ़ती जाती है, उसे उतनी ही अधिक आनन्द की उपलब्धि होती जाती है तथा अपने समस्त कर्म जीवमात्र के लिए समर्पित कर देने की भावना तीव्रतर होती जाती है-
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ॥
तात्पर्य यह है कि सभी लोग सुखी हों, निरोगी हों, कल्याणयुक्त हों। कोई भी दु:ख-कष्ट नहीं भोगे। इसी भावना से संचालित होकर सभी जीवों के कल्याण में रत रहना चाहिए। यही सर्वकल्याणमय भावना सन्तों का मुख्य लक्षण है; क्योंकि वे मन, वचन और काया से सदा परोपकार में लगे रहते हैं-
पर उपकार वचन मन काया। सन्त सहज सुभान खगराया ॥
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी के शब्दों में–
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे ,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।
अर्थात् जो अपने लिए जीता है वह पशु है, जो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी जीता है वह मनुष्य है और जो केवल दूसरों के लिए ही जीता है वह महामानव है, महात्मा है।
उपसंहार–परोपकारी अक्षय कीर्ति को धारण करते हैं। प्रत्येक युग में उनको सम्मान वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। महात्मा गाँधी, पं० मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खाँ, रामप्रसाद बिस्मिल आदि सदैव ही प्रातः स्मरणीय रहेंगे। तभी तो मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा है कि इस जीवन को अमर बनाने के लिए इसे दूसरों को समर्पित कर दो-
विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी ,
मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करें सभी ।
मानव का जीवन क्षणभंगुर है, किन्तु परोपकार के द्वारा वही अमरता को प्राप्त हो जाता है। भगवान् राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन राय “सर्वभूत हिते रतः’ रहकर ही अक्षय यश के भागी हैं।
वर्तमान समय में परोपकार का स्वरूप बदलता जा रहा है। परोपकार के आवरण में लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। कोई राजनीतिक नेता ‘गरीबी हटाओ’ का नारा लगाकर गरीबों का वोट अपनी ओर खींचता है तो कोई जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करवाकर अपना वोट बैंक पक्का करता है। कुछ व्यापारी आयकर में छूट पाने के लिए औषधालय खुलवाते हैं तथा पंजीकृत संस्थाओं में दान देते हैं। यह आज के परोपकार का परिवर्तित स्वरूप है। भारतीय संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’, ‘सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय’ के सविवेक का सन्देश देती है। आज ऐसी ही भावना की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति के इन सन्देशों को अपनाकर ही हम परोपकार के सर्वाधिक समीप पहुँच सकते हैं।
परोपकार किसी भी समाज एवं देश के सुख-संवर्धन का एकमात्र उपाय है। जिस समाज में परोपकारी लोगों का आधिक्य होगा वही सुखी और समृद्ध होगा। डॉ० हरिदत्त गौतम ‘अमर’ के शब्दों में –
पर उपकार निरत जो सज्जन कभी नहीं मरते हैं।
चन्द्र सूर्य जब तक हैं उन पर यशः पुष्प झरते हैं।
सांस्कृतिक प्रदूषण
सम्बद्ध शीर्षक
- समाज में नैतिक मूल्यों का विघटन
- केबिल टी०वी० के माध्यम से फैलता सांस्कृतिक प्रदूषण और हम
- भारतीय संस्कृति और दूरदर्शन [2010]
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- सांस्कृतिक प्रदूषण का अर्थ,
- सांस्कृतिक प्रदूषण का स्वरूप विचारों में प्रदूषण, कलाओं में प्रदूषण, दृष्टिकोण का प्रदूषण, खान-पान का प्रदूषण, रहन-सहन का प्रदूषण,
- उपसंहार।
प्रस्तावना–आज के वैज्ञानिक युग में हर ओर प्रदूषण की ही चर्चा है। खुली हवा, धूलरहित आवास, शान्त इमारतें और शोररहित सड़कें आज एक सपना बन कर रह गयी हैं। आज भी सावन आता है पर घरों में वह वृक्ष ही नहीं होता, जिस पर झूला डाला जा सके। घरों में वह खुला आँगन नहीं होता जहाँ बच्चों को हर्षध्वनि करते, भागते-दौड़ते देखा जा सके। आज द्रुतगति की आलीशान वातानुकूलित कारें तो हैं, परन्तु उसकी खिड़की खोलते ही बाहर का शोरगुल और गर्दगुबार बिना निमन्त्रण अन्दर घुसे आता है। आज बच्चे टी० वी० स्क्रीन का कार्टून अपने सपनों में देखते हैं और लोरी के स्थान पर सी० डी० अथवा ऑडियो टेप सुनते हुए सो जाते हैं। यही है–भौतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदूषण।
कुछ विद्वान् इसे विश्व की गम्भीरतम समस्या कहते हैं तो कुछ इसे मानवता का सबसे बड़ा शत्रु। आज सभी रोगों का मूल कारण प्रदूषण को ही माना जाता है तथा यह कहा जाता है कि इससे बच पाना असम्भव है। प्रदूषण सम्बन्धी कथन वास्तव में भौतिक पर्यावरण के प्रदूषण से ही सम्बन्धित है। भौतिक पर्यावरण प्रदूषण के अन्तर्गत मुख्य रूप से वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण, मृदा-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण ही आते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रदूषण केवल भौतिक पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, वरन् इसके कुछ अन्य रूप भी अति महत्त्वपूर्ण एवं चिन्ता के विषय हैं। प्रदूषण का एक अति गम्भीर रूप सांस्कृतिक प्रदूषण भी है। आज विश्व के अधिकांश विकासशील देश जहाँ एक ओर भौतिक प्रदूषण के शिकार हैं तो साथ-साथ ही वे गम्भीर सांस्कृतिक प्रदूषण के भी शिकार हो रहे हैं। भौतिक प्रदूषण के कारक, प्रभाव आदि स्पष्ट होते हैं तथा इनकी जाँच भी सरलता से की जा सकती है, परन्तु सांस्कृतिक प्रदूषण पर्याप्त सीमा तक छिपा हुआ होता है तथा यह अपना प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से डालता है। यद्यपि सांस्कृतिक प्रदूषण छिपा हुआ होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तथापि इसके परिणाम अति गम्भीर, हानिकारक तथा दूरगामी होते हैं।
सांस्कृतिक प्रदूषण का अर्थ-प्रदूषण का सामान्य अर्थ है-किसी स्थापित व्यवस्था के मूल रूप में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन होना जो जनसामान्य के लिए सामान्य रूप से हानिकारक हो। इस मापदण्ड के आधार पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने या ऑक्सीजन की मात्रा घटने की स्थिति वायु-प्रदूषण की स्थिति होती है। सांस्कृतिक प्रदूषण के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि किसी संस्कृति की मौलिक विशेषताओं एवं लक्षण में उससे भिन्न तत्त्वों का समावेश हो जाना ही सांस्कृतिक प्रदूषण है। सांस्कृतिक प्रदूषण के पूर्व संस्कृति के अर्थ को स्पष्टरूपेण समझना आवश्यक है। संस्कृति की अवधारणा पर्याप्त जटिल है। वास्तव में किसी समाज द्वारा जो कुछ भी अपने पूर्व-पुरुषों के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वह सब कुछ संस्कृति ही है। संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कलाएँ, नीति, विधि, रीति-रिवाज तथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताओं एवं आदतों को सम्मिलित किया जाता है। वस्तुतः संस्कृति जीवन का एक ढंग है, जो सैकड़ों-हजारों वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होता है।
वर्तमान वैज्ञानिक युग में विश्व के सभी देशों एवं भागों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बहुपक्षीय सम्पर्क स्थापित होने लगे हैं। दूरसंचार के साधनों, यातायात की सुविधाओं, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन, इण्टरनेट आदि के माध्यम से अब विश्व की समस्त संस्कृतियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करने लगी हैं। इस स्थिति में विकसित (पाश्चात्य) देशों ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विकासशील देशों पर थोपना प्रारम्भ कर कर दिया है। इसी सांस्कृतिक होड़ से हमारे देश की संस्कृति गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही है। हमारी संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, वह हमारी मूल संस्कृति के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अतः इस प्रकार से होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन को हम सांस्कृतिक प्रदूषण की संज्ञा देते हैं।
सांस्कृतिक प्रदूषण का स्वरूप-वर्तमान परिस्थितियों में सांस्कृतिक प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान दूरदर्शन के विदेशी और कुछ-एक देशी चैनेलों का है। एम टी० वी०, वी टी० वी०, जी टी० वी० तथा कुछ अन्य विदेशी चैनेल सांस्कृतिक प्रदूषण के मुख्य माध्यम बने हुए हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण के मुख्य रूपों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है|
(1) विचारों में प्रदूषण–पारम्परिक भारतीय संस्कृति में शुद्ध विचारों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में पाश्चात्य सांस्कृतिक संघात के कारण यह भारतीय धारणा क्रमश: परिवर्तित हो रही है। अब सामान्य जनमानस की विचारधारा धीरे-धीरे कुत्सित हो रही है, विचारों में तीव्र उथल-पुथल मची हुई है तथा व्यक्ति की विचारशक्ति भ्रमित हो रही है। विचारों का इस प्रकार से विकृत होना सांस्कृतिक प्रदूषण का ही एक रूप है।
(2) कलाओं में प्रदूषण- भारतीय कलाओं की अपनी कुछ विशेषताएँ थीं। ये कलाएँ आदर्शोन्मुखी थीं। पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भारतीय कलाओं में कुछ ऐसा तीव्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि सांस्कृतिक प्रदूषण को ही दर्शाता है। साहित्य में दुःखान्त रचनाओं को महत्त्व देना, अकहानी तथा अकविता का प्रचलन, प्रयोगवादी काव्य का प्रादुर्भाव आदि साहित्य के क्षेत्र में प्रदूषण कहे जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में सूक्ष्म कला या एब्स्ट्रैक्ट आदि अपने आप में एक प्रदूषणकारी प्रचलन ही हैं। संगीत के क्षेत्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अवहेलना करके पॉप संगीत तथा डिस्को संगीत स्पष्ट रूप से भारतीय संगीत के लिए प्रदूषण का ही काम कर रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का अत्यल्प विकृत रूप सिने-संगीत के रूप में श्रोताओं में पर्याप्त लोकप्रिय था। लेकिन अब इस संगीत के दृश्य-श्रव्य माध्यम को विदेशी वाद्यों तथा पर्याप्त नग्नता का समावेश कर रीमिक्स की नवीन संज्ञा देकर पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे भी सांस्कृतिक प्रदूषण का ही स्वरूप माना जाना चाहिए। नृत्य के क्षेत्र में भी कत्थक, भरतनाट्यम आदि भारतीय नृत्यों को छोड़कर पाश्चात्य नृत्यों को अपनाना प्रदूषणकारी ही है। वर्तमान समय में तो भारतीय लोक-नृत्यों का भी पश्चिमीकरण होता जा रहा है। पंजाब का लोकप्रिय लोक-नृत्य भाँगड़ा आज विदेशी रंग में रँगता दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन सांस्कृतिक प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाद्य-यन्त्रों में भी अब भारतीय वाद्य-यन्त्र अनावश्यक-से प्रतीत हो रहे हैं तथा पाश्चात्य इलेक्ट्रॉनिक वाद्य-यन्त्र अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।
(3) दृष्टिकोण का प्रदूषण–पारम्परिक रूप से भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक तथा नैतिकता की ओर उन्मुख था, परन्तु अब पाश्चात्य सांस्कृतिक संघात ने भारतीय जनसामान्य के दृष्टिकोण को भी भौतिकवादी बना दिया है। सम्मिलित परिवारों की भारतीय अवधारणा अब धीरे-धीरे विघटित परिवारों का रूप लेने लगी है। सांस्कृतिक प्रदूषण के कारण ही नवयुवकों में अब बड़े-बुजुर्गों के प्रति सम्मान की वह भावना नहीं रह गयी, जो पहले पायी जाती थी। आज प्रत्येक बात में भौतिकवादी दृष्टिकोण से लाभ-हानि को ही प्राथमिकता दी जाती है। पारम्परिक दृष्टिकोण में होने वाला यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक प्रदूषण ही है।
(4) खान-पान का प्रदूषण-खान-पान को भी सांस्कृतिक मान्यता के अन्तर्गत ही माना जाता है। वर्तमान समय में इस सांस्कृतिक मान्यता में भी तीव्र तथा गम्भीर परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। आज हर कोई विदेशी खाद्य-पदार्थों तथा पकवानों को अधिक पसन्द कर रहा है। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पंजाबी, कश्मीरी आदि व्यंजनों के स्थान अब चाइनीज़, फास्ट फूड्स, बर्गर, पिज़ा आदि ने ले लिये हैं। भारतीय परिवारों में विवाह आदि शुभ अवसरों पर विदेशी व्यंजनों का परोसा जाना अब शान की बात समझी जाती है। खान-पान में होने वाला यह परिवर्तन भी सांस्कृतिक प्रदूषण ही है।
(5) रहन-सहन का प्रदूषण–आज हर भारतीय परिवार पाश्चात्य-प्रतिमान को आदर्श रहन-सहन मानता है। पारम्परिक भारतीय रहन-सहन को अब दकियानूसी माना जाने लगा है। रसोईघर, बैठक, शयन-कक्ष, पहनावा, सौन्दर्य प्रसाधन आदि सभी स्थानों पर पाश्चात्य प्रतिमानों को ही अपनाया जा रहा है, यह सांस्कृतिक जीवन का ही प्रदूषण है।
उपसंहार-निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हमारा समाज घोर सांस्कृतिक प्रदूषण का शिकार हो रहा है। इस सांस्कृतिक प्रदूषण के गम्भीर परिणाम हो रहे हैं। हमारे परिवार विघटित हो रहे हैं, विवाह-विच्छेद हो रहे हैं, मान्यताएँ बदल रही हैं तथा परम्पराएँ छिन्न-भिन्न हो रही हैं। स्वास्थ्य-हीनता और नैतिक मूल्यों-मर्यादाओं के टूटने के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। यदि सांस्कृतिक प्रदूषण की इस आँधी को समय रहते रोका न गया तो निकट भविष्य में हम अपनी पहचान गंवा बैठेंगे। हम ने घर के रहेंगे और न घाट के। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक विशेष रूप से युवाओं तथा शिक्षकों का दायित्व है कि वे विदेशियों द्वारा फैलायी जा रही अपसंस्कृति अथवा सांस्कृतिक प्रदूषण का विरोध करें तथा इससे अपने समाज एवं देश को बचाने का प्रयास करें।
नैतिक मूल्यों का हास : कारण एवं निवारण (2016)
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- प्रतिभा की उपेक्षा,
- वैचारिक प्रदूषण,
- पश्चिम की नकल,
- रोजगार की समस्या,
- भ्रष्ट राजनीतिक विरासत,
- समस्याओं/कारणों के निवारण के उपाय,
- उपसंहार।
प्रस्तावना-चाहे धर्म का क्षेत्र हो या दर्शन का, चाहे कला का क्षेत्र हो या विज्ञान का, शताब्दियों तक हमारा देश, विश्व के मानचित्र पर जगमगाता रहा, और आज भी यह दुनिया के उन महानतम देशों में से एक है, जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं है। आज विश्वभर में फैले हुए भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर सफलता के ऊँचे शिखर को नैतिक मूल्यों के कारण छू रहे हैं। और यह भी कि–आज अमेरिका की 70 प्रतिशत सिलीकॉन वैली पर भारतीयों का कब्जा है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि आज हमारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण अब हमारी छवि दुनिया में धूमिल होने लगी है। नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण हमारी नई पीढ़ी जब इस प्रकार की विरोधाभासी व्यवस्था के बीच से होकर गुजर रही हो, तो उसकी दशा और दिशा का सही अनुमान लगा पाना तो बहुत कठिन है, परन्तु सम्भावित अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रतिभा की उपेक्षा–जाति-आधारित आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से प्रतिभा और दक्षता का अनादर हो रहा है। प्रोन्नतियों में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, परन्तु वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की गयी। यह प्रतिभा और योग्यता के साथ किया जाने वाला अन्याय है और यह अन्याय केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण किया गया है। ठीक है कि गरीबों और पिछड़ों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए परन्तु इसके लिए उन्हें योग्य एवं प्रतिभाशाली बनाने के उपाय किये जाने चाहिए। आरक्षण की बैसाखी से नई पीढ़ी की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है और फिर गरीब और पिछड़े तो हर जाति में होते हैं। यदि आरक्षण ही देना है तो फिर उन सभी को देना चाहिए, परन्तु वोट बैंक के लाभ-हानि देखकर चुन-चुनकर अपने पक्ष की कुछ विशेष जातियों के लोगों को ही आरक्षण देना और बाकी गरीबों और पिछड़ों को उनके अपने हाल पर छोड़ देना तनिक भी उचित नहीं है। देखा यह भी गया है कि इस आरक्षण का लाभ, पिछड़ों में जो सम्पन्न लोग हैं, उन्हीं को मिल सका है। शेष की हालत बदस्तूर है। यदि निजीक्षेत्र में भी आरक्षण किया गया, यदि विधानसभाओं और संसद में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हो गया, तो स्थिति और अधिक विकट हो जाएगी। ऐसा करने से नई पीढ़ी की दशा बदतर होगी और दिशा भयावह।।
वैचारिक प्रदूषण-नई पीढ़ी को जो विचार उत्तराधिकार में मिल रहे हैं, वे सामाजिक एकता और सद्भाव को बनाये रखने वाले अथवा सर्वधर्म समभाव वाले नहीं हैं। समाज को जोड़ने के बदले सर्वत्र अलगाव और बिखराव ही अधिक दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्र की एकता और अखण्डता को जाति, धर्म, सम्प्रदाय, बोली, भाषा और क्षेत्र के आधार पर कई टुकड़ों में बाँटने के प्रयास जारी हैं, और यह सब वोट बैंक की राजनीति के कारण हुआ है। यही कारण है कि अयोध्या में विवादित ढाँचा गिराये जाने के आठ वर्ष बाद भी तेरहवीं लोकसभा का सत्र हफ्ते भर तक नहीं चलने दिया गया। एक ही देश में कहीं शौर्य दिवस और कहीं कलंक दिवस मनाये जाने के पीछे यह वैचारिक प्रदूषण ही मुख्य कारण है। इसी वैचारिक प्रदूषण के कारण राजनीतिक दल अपने स्वार्थ को राष्ट्रीय आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते हैं। ऐसे प्रदूषित विचारों के मध्य जी रही नई पीढ़ी की दशा और दिशा उज्ज्वल होने की सम्भावना कम ही है।
पश्चिम की नकल-देश की नई पीढ़ी पश्चिम की नकल करते-करते अपनी अकल भी गॅवाती हुई दीख रही है। भारतीय जीवन-दर्शन, भारतीय जीवन-मूल्य, भारतीय आदर्श और भारतीय संस्कृति से अपना पल्ला झाड़कर, यही पीढ़ी पाश्चात्य भौतिकवादी और भोगवादी संस्कृति की ओर उन्मुख दिखाई देती है। नई पीढ़ी की लड़कियों के शरीर पर कपड़े घटते जा रहे हैं और सौन्दर्य प्रसाधनों के बाजारों में भीड़ उमड़ती जा रही है। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के नाम पर नग्नता और अश्लीलता परोसी जा रही है। लड़के भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं हैं। शास्त्रीय संगीत के बदले पॉप म्यूजिक लोकप्रिय होता जा रहा है। खुलेपन और प्रगतिशील होने के नाम पर टी०वी० चैनल भी घर-घर में नग्नता और अश्लीलता ही परोस रहे हैं। यह सब देखकर मुझे तो नहीं लगता कि नई पीढ़ी की दशा और दिशा अच्छी हो सकेगी।
रोजगार की समस्या-यद्यपि नई पीढ़ी सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जी रही है, परन्तु उसके लिए साधन जुटाना नई पीढ़ी के लिए आसान काम नहीं है। सरकारी नौकरियाँ बहुत कम हैं क्योंकि अब अधिकतर काम कम्प्यूटर करने लगे हैं। फिर आरक्षण भी इसमें बाधक है और हमारी शिक्षा नीति भी रोजगारपरक नहीं है। राजनीतिज्ञों की सन्तानें तो विदेशों में अच्छी उपयोगी शिक्षा पा रही हैं पर देश की सामान्य जनता के लिए सरकारी स्कूल भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। जो विद्यालय हैं भी वहाँ गणित, विज्ञान और भाषा आदि विषयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भारी कमी है। आज की शिक्षा-व्यवस्था स्नातक बनाने के बाद छात्र में शारीरिक परिश्रम के प्रति निष्ठा नहीं जगाती, बल्कि छात्र न घर का रहता है न घाट की। ऐसी दशा में नई पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखाई देता है। उद्योग लगाने के लिए पूँजी की जरूरत होती है, परन्तु वह पूँजी आयेगी कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर पाना बहुत कठिन है।
भ्रष्ट राजनीतिक विरासत-आजादी के बाद छः दशकों में जैसी धोखाधड़ी भारतीय जनता के साथ की गई, उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। जनता के धन को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस लूट में राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जिम्मेदार रहे हैं। भारत के गृह सचिव एन०एन० बोहरा ने 1995 में अपनी रिपोर्ट में कहा था-“माफिया संगठनों को एक तन्त्र देश में समानान्तर सरकार चला रहा है। और उसने राज्य के उपकरणों को अप्रासंगिक बना दिया है। अपराधी गिरोहों, तस्कर गिरोहों और आर्थिक लॉबियों का तेजी से विस्तार हुआ है।”
समस्याओं/कारणों के निवारण के उपाय-राष्ट्र की भौतिक दशा सुधारने के लिए नैतिक मूल्यों का उपयोग कर हम उन्नति की सही राह चुन सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में लोगों के बीच फैला भ्रष्टाचार किस तरह से विकास की धार को मोथरा (कुंद) किए हुए है।
नैतिक मूल्यों में ह्रास होने से समाज में हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि मूल्यविहीन समाज में असन्तोष फैल रहा है। बेकारी के बढ़ने से युवक असन्तोष जैसी कई प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी दिखाई देती हैं। छोटे से बड़े नौकरशाह निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के अंधकूप में डुबकियाँ लगा रहे हैं, उन्हें समाज या राष्ट्र की कोई परवाह नहीं है। इन परिस्थितियों से देश को उबारने के लिए आत्ममंथन अनिवार्य हो जाता है। नैतिक मूल्यों के द्वारा ही देश को समस्याओं के गर्त से उबारा जा सकता है, क्योंकि नीति से ही नैतिक शब्द बना है जिसका अर्थ है-सोच-समझकर बनाए गए नियम या सिद्धान्त। अतः अपने हृदय से दूषित भावनाओं का त्याग कर तथा सदाचार की वैसी बातें जो सभी धर्मों व सभी सम्प्रदायों को मान्य हैं, समाहित कर हम प्रगतिशील समाज की रचना कर सकते हैं तथा साथ ही नैतिक मूल्यों का उत्थान भी कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों के ह्रास का निवारण तभी सम्भव हो सकता है जब हम अपनी संस्कृति को पहचानें, उसे अपने जीवन में उतारे और पश्चिम की ओछी भोगवादी संस्कृति से प्रभावित न हों।
उपसंहार-निश्चय ही जिस समाज में अपराधी लोग, जातीय गौरव के रूप में शोभित हो रहे हैं, तो राजनीतिक दल उनसे वंचित कैसे रह सकते हैं? सवाल यह भी है कि जिन लोगों पर गम्भीर आरोप हैं वे चुनाव कैसे जीत जाते हैं? वास्तव में राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण ही राजनीति के अपराधीकरण की समस्या पैदा हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो चन्दन तस्कर वीरप्पन दो राज्य सरकारों को अपने इशारे पर नाच नहीं नचाता। यही कारण है कि आज तमाम विकास योजनाओं का लाभ नेता, अधिकारी, इंजीनियर, बैंक मैनेजर और दलाल उठा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे शासक जिस दिन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सफल होंगे, उसी दिन से नई पीढ़ी की दशा और दिशा प्रकाशित होने लगेगी; तभी हमारी संस्कृति और समाज का उत्थान हो सकेगा।
आधुनिक जीवन में संचारमाध्यमों की उपयोगिता
सम्बद्ध शीर्षक
- शिक्षा के उन्नयन में संचय माध्यमों की उपयोगिता [2010]
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- संचारमाध्यमों का मानव-जीवन में महत्त्व,
- उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में संचारमाध्यमों का योगदान,
- भारत में संचारमाध्यमों का विकास (i) समाचार-पत्र, (ii) रेडियो, (ii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, (iv) इण्टरनेट सेवा,
- उपसंहार
प्रस्तावना--अपने विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को सम्प्रेषित करने के लिए मनुष्य को संचारमाध्यम की आवश्यकता पड़ती है। संचार का माध्यम मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। पहले मनुष्य आपस में बोलकर या इशारे से अपनी अभिव्यक्ति करता था। वैज्ञानिक प्रगति ने उसे संचार-माध्यम के अन्य साधन भी उपलब्ध करवाए। अब मनुष्य दुनिया के एक छोर पर मौजूद व्यक्ति से दुनिया के दूसरे छोर से वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बात करने में सक्षम है।
ये वैज्ञानिक उपकरण ही संचार के माध्यम कहलाते हैं। टेलीफोन, रेडियो, समाचार-पत्र, टेलीविजन इत्यादि संचार के ऐसे ही माध्यम हैं। टेलीफोन ऐसा माध्यम है, जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है, किन्तु संचार के कुछ माध्यम ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से एक साथ कई व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। जिन साधनों का प्रयोग कर एक बड़ी जनसंख्या तक विचारों, भावनाओं व सूचनाओं को सम्प्रेषित किया जाता है उन्हें हम संचार के माध्यम कहते हैं।
संचार-माध्यमों का मानव-जीवन में महत्त्व-मानव-जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में संचारमाध्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूचनाओं के आदान-प्रदान करने में समय की दूरी घट गई है। अब क्षणभर में संदेश व विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन तथा उद्योग आदि के क्षेत्र में संचारमाध्यम का महत्त्व बढ़ गया है। अपराधों पर नियंत्रण करने तथा शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में संचार माध्यम का विशेष योगदान है। संचारमाध्यम के अभाव में देश में शान्ति और सुव्यवस्था करना कठिन कार्य है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी सही सूचनाओं का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है; अतः कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के संचारमाध्यम की व्यवस्था का विकसित होना अत्यावश्यक है।
उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में संचारमाध्यमों का योगदान–किसी भी देश का विकास उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाता है; लेकिन सफल व्यवसाय और उद्योगों के विकास के लिए संचार माध्यम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। भूमण्डलीकरण के इस काल में तो व्यवसायी एवं उद्योगपति सूचनाओं के माध्यम से व्यवसाय एवं उद्योग में नई ऊँचाइयों को छूने के लिए लालायित हैं। सूचनाएँ व्यवसाय का जीवन-रक्त हैं। व्यवसाय के अन्तर्गत माल के उत्पादन से पूर्व, उत्पादन से वितरण तक और विक्रयोपरान्त सेवाएँ प्रदान करने के लिए संचार माध्यम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार, संचार-माध्यम एवं सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत अग्रणी देश बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 में दक्षिण एशिया में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का हिस्सा 76 प्रतिशत था। चीन में भारत से ज्यादा मोबाइल फोन हैं, लेकिन इण्टरनेट के क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को लाभ उठाने के लिए भारत का माहौल चीन से कहीं बेहतर है। संचार माध्यम में क्रान्ति ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नई सम्भावना को जन्म दिया है, जिसका लाभ विकसित और विकासशील देश दोनों ही उठा रहे हैं।
भारत में संचारमाध्यमों का विकास–भारत ने संचार माध्यम के क्षेत्र में असीमित उन्नति की है। भारत का संचार नेटवर्क एशिया के विशालतम संचार नेटवर्कों में गिना जाता है। जून, 2013 के अन्त तक 903.10 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के साथ भारतीय दूरसंचार नेटवर्क चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। जून, 2013 के अन्त तक 873.37 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के साथ भारतीय वायरलैस टेलीफोन नेटवर्क भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज लगभग सभी देशों के लिए इण्टरनेशनल सबस्क्राइबर डायलिंग सेवा उपलब्ध है। इण्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 7 करोड़ 34 लाख है। अन्तर्राष्ट्रीय संचार-क्षेत्र में उपग्रह संचार और जल के नीचे से स्थापित संचार सम्बन्धों द्वारा अपार प्रगति हुई है। ध्वनि वाली और ध्वनिरहित संचार सेवाएँ, जिनमें आँकड़ा प्रेषण, फैसीपाइल, मोबाइल रेडियो, रेडियो पेनिंग और लीज्ड लाइन सेवाएँ शामिल हैं। 31 मार्च, 2013 ई० की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 357.74 मिलियन फोन हैं।
जनसंचार माध्यमों को कुल तीन वर्गों-मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम एवं नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रण माध्यम के अन्तर्गत समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पैम्फलेट, पोस्टर, जर्नल पुस्तकें इत्यादि हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्में आती हैं। और इण्टरनेट जनसंचार का नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-
(i) समाचार-पत्र—मुद्रण माध्यम की शुरुआत गुटेनबर्ग द्वारा 1454 ई० में मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ हुई थी। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। आज समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ विश्वभर में जनसंचार का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसे फटाफट साहित्य का नाम दिया था। समाचार-पत्र कई प्रकार के होते हैं-त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक। इस समय विश्व के अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या अन्य प्रकार के पत्रों से अधिक है। भारत का पहला समाचार-पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ‘बंगाल गजट’ था। इसका प्रकाशन 1780 ई० में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। हिन्दी का पहला समाचार-पत्र ‘उदन्त मार्तण्ड’ था। इस समय भारत में कई भाषाओं के लगभग तीस हजार से भी अधिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र ‘द टाइम्स ऑफ इण्डिया’, ‘द हिन्दू’, ‘द : हिन्दुस्तान टाइम्स’ इत्यादि हैं। हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्रों में दैनिक जागरण’, दैनिक भास्कर’, ‘हिन्दुस्तान’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘नई दुनिया’, ‘जनसत्ता’ इत्यादि प्रमुख हैं। समाचार-पत्र की उपयोगिता महात्मा गाँधी के इस कथन से भी उजागर होती है-“समाचार-पत्र सच्चाई अथवा वास्तविकता को जानने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।’
(ii) रेडियो-आधुनिक काल में रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख साधन है, विशेष रूप से दूरदराज के उन क्षेत्रों में जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या जिन क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत में वर्ष 1923 में रेडियो के प्रसारण के प्रारम्भिक प्रयास और वर्ष 1927 में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत के बाद अब तक इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हासिल की जा चुकी है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण-एफएम रेडियो प्रसारण है। ‘एफएम’ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा रेडियो प्रसारण है, जिसमें आवृत्ति को प्रसारण ध्वनि के अनुसार मॉड्यूल किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। स्थानीय स्तर पर ‘एफएम’ प्रसारण के लाभ को देखते हुए देश के कई विश्वविद्यालयों ने इसके माध्यम से अपने शैक्षिक प्रसारण के उद्ददेश्य से अपने-अपने एफएम प्रसारण चैनलों की शुरुआत की है। यही कारण है कि इससे न केवल आम जनता को लाभ पहुँचा है, बल्कि दूरस्थ एवं खुले विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए भी यह अति लाभप्रद सिद्ध हुआ है। आज एफएम प्रसारण दनियाभर में रेडियो प्रसारण का पसन्दीदा माध्यम बन चुका है, इसका एक कारण इससे उच्च गुणवत्तायुक्त स्टीरियोफोनिक आवाज की प्राप्ति भी है। शुरुआत में इस प्रसारण की देशभर में कवरेज केवल 30% थी, किन्तु अब इसकी कवरेज बढ़कर 60% से अधिक तक जा पहुँची है।
(iii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा–सभी महानगरों और 29 राज्यों के लगभग सभी शहरों के लिए सेवाएँ शुरू हो चुकी हैं। 31 मई, 2013 ई० तक देश में 873.37 मिलियन सेल्यूलर उपभोक्ता थे। नई दूरसंचार नीति के अन्तर्गत सेल्यूलर सेवा के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 1 अगस्त, 1999 ई० से राजस्व भागीदारी प्रणाली अपनाने की अनुमति मिल गई। देश के विभिन्न भागों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा चलाने के लिए एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० को लाइसेंस जारी किए गए। नई नीति के अनुसार सेल्यूलर ऑपरेटरों को यह छूट दी गई कि वे अपने कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार की मोबाइल सेवा, जिसमें ध्वनि और गैर-ध्वनि संदेश शामिल हैं, डेटा सेवा और पी०सी०ओ० उपलब्ध करा सकते हैं।
(iv) इण्टरनेट सेवा–नवम्बर, 1998 ई० से इण्टरनेट सेवा निजी भागीदारी के लिए खोल दी गई। इसके बाद सरकार ने देश की प्रत्येक पंचायत में वर्ष 2012 में ब्रॉडबैण्ड की शुरुआत करने का निर्णय लिया। समयानुसार इण्टरनेट आम आदमी की निजी और व्यावसायिक जिन्दगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लगभग सभी व्यावसायिक साइटों को इण्टरनेट पर लांच किया जा चुका है। ई-मेल द्वारा मास कैम्पेन चलाना अब एक सामान्य प्रचलन हो चुका है। ‘चैट’ एक ऐसी उपलब्ध सेवा है, जिसके द्वारा इण्टरनेटधारक एक-दूसरे के साथ आपस में ऑनलाइन वार्तालाप कर सकते हैं। ई-गर्वनेंस सरकार की पहली प्राथमिकता है।
उपर्युक्त संचार के माध्यमों के प्रमुख कार्य हैं-लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार, भ्रष्टाचार एवं घोटालों का पर्दाफाश तथा समाज की सच्ची तसवीर प्रस्तुत करना। इन माध्यमों से लोगों को देश की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। किसी भी देश में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष एवं निर्भीक संचार माध्यमों का होना आवश्यक है। ये देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
चुनाव एवं अन्य परिस्थितियों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जन-साधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी संचारमाध्यमों को ही वहन करनी पड़ती है। ये सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इसे हम मीडिया भी कहते हैं। जनता की समस्याओं को इन माध्यमों से जन-जन तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर ये देश एवं समाज का भला करते हैं। इस तरह, ये आधुनिक समाज में लोकतन्त्र के प्रहरी का रूप ले चुके हैं, इसलिए इन्हें लोकतन्त्र के चतुर्थ स्तम्भ की संज्ञा दी गई है। आशा है, आने वाले वर्षों में भारतीय मीडिया अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए देश के विकास में और सहयोग करेगा।
उपसंहार–वास्तव में संचारमाध्यम (प्रणाली) ने विश्व की दूरियों को समेटते हुए मानव-जीवन को एक नया मोड़ दिया है। आज हमारा देश संचार टेक्नोलॉजी की दौड़ में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। विभिन्न निजी कम्पनियों को भी इसमें विशेष योगदान रहा है, जिसके कारण हम इसे देश के कोने-कोने से जोड़ने में सफल हुए हैं। इस प्रकार संचारमाध्यम के प्रसार ने शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, व्यवसाय तथा उद्योग के विकास के साथ-साथ मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति को गति प्रदान की है।
स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता
सम्बद्ध शीर्षक
- स्वच्छता अभियान [2016, 18]
प्रमुख विचार-बिन्दु–
- प्रस्तावना,
- मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना,
- स्वच्छता अभियान की शुरुआत,
- स्वच्छता अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा,
- स्वच्छता अभियान का प्रारूप-(i) शहरी क्षेत्रों के लिए, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, (ii) विद्यालयों के लिए,
- उपसंहार।
प्रस्तावना–‘स्वच्छता अभियान’ एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गाँधी जी की 145वीं जयन्ती के अवसर पर माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस अभियान के आरम्भ की घोषणा की। यह अभियान प्रधानमन्त्री जी की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। 2 अक्टूबर, 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूह को सम्बोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छता अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की। साफ-सफाई के सन्दर्भ में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है।
साफ-सफाई को लेकर दुनिया भर में भारत की छवि बदलने के लिए प्रधानमन्त्री जी बहुत गम्भीर हैं। उनकी इच्छा स्वच्छता अभियान को एक जन-आन्दोलन बनाकर देशवासियों को गम्भीरतापूर्वक इससे जोड़ने की है। हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गाँधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ लगाई। कहा जाता है। कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गाँधी जी का सबसे प्रिय स्थान था। वे अक्सर यहाँ आकर ठहरते थे।
इसके बाद मोदी जी ने जनपथ जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मिनट का भाषण दिया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गाँधी और लालबहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनों महापुरुषों को इस अभियान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा-“गाँधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था, ‘क्विट इण्डिया क्लीन इण्डिया। आजादी की लड़ाई में उनका साथ देकर देशवासियों ने ‘क्विट इण्डिया’ के सपने को तो साकार कर दिया, लेकिन अभी उनका ‘क्लीन इण्डिया का सपना अधूरा है।”
मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना-माननीय मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना यह है कि देश के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण परिवार में एक स्वच्छ शौचालय हो, जिन घर-परिवारों में स्थानाभाव के कारण शौचालय बनाया जाना सम्भव न हो, वहाँ पर सुलभ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए। देश के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए स्वच्छ और पृथक्-पृथक् शौचालय हों। उनकी इस संकल्पना से जहाँ सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा समाप्त होगी, वहीं देश की उन करोड़ों महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा, जिनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। उन बालिकाओं के विद्यालय जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो विद्यालयों में अलग शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय नहीं जा पातीं।
मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना केवल शौचालयों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। उनका प्रयास है कि देश का प्रत्येक कोना स्वच्छ हो। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक की भागेदारी आवश्यक है। उन्होंने देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों का आह्वान किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि वह न स्वयं गन्दगी फैलाएगा और न दूसरों को फैलाने देगा। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इस जिम्मेदारी को समझे तो देश गन्दा ही न होगा और सारा देश स्वत: ही स्वच्छ हो जाएगा। | स्वच्छता अभियान की शुरुआत-स्वच्छता अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने महात्मा गाँधी जी की जयन्ती पर 2 अक्टूबर, 2014 ई० को राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। इस दिन उन्होंने स्वयं मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर झाडू लगाकर फुटपाथ की सफाई की और स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बने पहले जैविक शौचालय (बायो टॉयलेट) को जनता को समर्पित किया।
स्वच्छता अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा–स्वच्छता अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री जी ने 2 अक्टूबर को ही देश के नौ प्रतिष्ठित लोगों को नवरत्नों के रूप में नामांकित किया, जिनसे प्रेरणा ग्रहण करके देश के लोग स्वच्छता अभियान में पूर्ण मनोयोग से लग जाएँ। उनके ये नवरत्न हैं—अनिल अम्बानी, सचिन तेन्दुलकर, सलमान खान, प्रियंका चौपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर और शाजिया इल्मी। इसके अलावा उन्होंने टी०वी० सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की सम्पूर्ण टीम को भी नामित किया है।
इसी प्रकार, 7 नवम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के असी घाट पर मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के नवरत्नों के रूप में भी नौ प्रसिद्ध लोगों को नामांकित किया। इन नौ लोगों में प्रदेश के मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव, क्रिकेटर मुहम्मद कैफ तथा सुरेश रैना, हास्य टी०वी० कलाकार राजू श्रीवास्तव, सूफी गायक कैलाश खेर, भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, लेखक मनु शर्मा, संस्कृत विद्वान् पद्मश्री प्रोफेसर देवीप्रसाद द्विवेदी, आन्ध्र विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति जगद्गुरु रामभद्राचार्य सम्मिलित हैं।
मोदी जी ने इन लोगों के नामांकन के साथ इन सभी का आह्वान किया कि ये सभी लोग अपने स्तर पर नौ-नौ और लोगों को इस अभियान हेतु नामांकित करें, फिर वे लोग दूसरे नौ-नौ लोगों को नामांकित करें। इस प्रकार लोगों की एक श्रृंखला बनती चली जाएगी और देश के सभी लोग इस अभियान से जुड़कर भारत को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे।
स्वच्छता अभियान का प्रारूप-स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया गया जन-आन्दोलन है, जिसका प्रयास सन् 2019 तक सम्पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। सरकारी सहायता हेतु इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है-
(i) शहरी क्षेत्रों के लिए अभियान का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना तथा पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम पाँच साल की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खुले में शौच करने को रोकना, स्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के सम्बन्ध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कार्यक्रम शामिल हैं।
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए माँग-आधारित एवं जन-केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्वसुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराना शामिल है, जिससे ग्रामीणों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अभियान का उद्देश्य पाँच वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे को इस्तेमाल उसे पूँजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करे – लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध-स्तर पर प्रारम्भ कर ग्रामीण आबादी और कूल शिक्षकों व छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत, समिति और जिला परिषद् को भी इससे जोड़ा जाना है।
(iii) विद्यालयों के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधीन स्वच्छ विद्यालय अभियान 25 सितम्बर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 ई० के बीच केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में आयोजित किया गया। इस दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ इस प्रकार रहीं–
- शिक्षकगण स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर, विशेष रूप से महात्मा गाँधी जी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के सम्बन्ध में बात करें।
- कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना।
- स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना और इनकी मूर्तियों की सफाई करना।
- शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना।
- रसोई और भण्डार-गृह की सफाई करना।
- स्कूल एवं बगीचों का रख-रखाव और सफाई करना।
- खेल के मैदान की सफाई करना।
- स्कूल-भवन का वार्षिक रख-रखाव, रँगाई एवं पुताई के साथ।
- निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- बाल मन्त्रिमण्डलों का निगरानी दल बनाना और सफाई अभियान की निगरानी करना।
इसके अलावा फिल्म-शो, स्वच्छता पर निबन्ध/पेन्टिग और अन्य प्रतियोगिताओं, नाटकों आदि के आयोजन द्वारा स्वच्छता एवं अच्छे स्वास्थ्य का सन्देश प्रसारित करना। मन्त्रालय ने इसके अलावा स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सप्ताह में दो बार आधे घण्टे सफाई अभियान शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा।
उपसंहार—आशा की जा सकती है कि स्वच्छता अभियान की संकल्पना निश्चय ही साकार होगी; क्योंकि जिस अभियान के प्रणेता माननीय नरेन्द्र मोदी जैसे कर्मठ, श्रमशील, ईमानदार और राष्ट्रवादी व्यक्ति हों उसकी सफलता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यह अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाएगा उस दिन न केवल कश्मीर, वरन् सम्पूर्ण भारत देश धरती का स्वर्ग कहलाएगा।
मानव-जीवन में योग शिक्षा का महत्त्व
सम्बद्ध शीर्षक
- योग शिक्षा : आवश्यकता और उपयोगिता (2016)
रूपरेखा-
- प्रस्तावना,
- योग का अर्थ,
- योग की आवश्यकता,
- योग की उपयोगिता,
- योग के सामान्य नियम
- योग से लाभ,
- उपसंहार।।
प्रस्तावना-योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन या स्थिति में रखना जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। योगासन शरीर की आन्तरिक प्रणाली को गतिशील करता है। इससे रक्त-नलिकाएँ साफ होती हैं तथा प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है जिससे उनमें स्फूर्ति आती है। परिणामत: व्यक्ति में उत्साह और कार्य-क्षमता का विकास होता है तथा एकाग्रता आती है।
योग का अर्थ-योग, संस्कृत के यज् धातु से बना है, जिसका अर्थ है, संचालि। ५५ म्वद्ध करना, सम्मिलित करना अथवा जोड़ना। अर्थ के अनुसार विवेचन किया जाए तो शरीर एवं आत्मा का मि : ही योग कहलाता है। यह भारत के छः दर्शनों, जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है, में से एक है। अन्य दर्शन हैं-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त एवं मीमांसा। इसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 ई०पू० में हुई थी। पहले यह विद्या गुरु-शिष्य परम्परा के तहत पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती थी। लगभग 200 ई०पू० में महर्षि पतञ्जलि ने योग-दर्शन को योग-सूत्र नामक ग्रन्थ के रूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए महर्षि पतञ्जलि को ‘योग का प्रणेता’ कहा जाता है। आज बाबा रामदेव ‘योग’ नामक इस अचूक विद्या का देश-विदेश में प्रचार कर रहे हैं।
योग की आवश्यकता–शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। इसके स्वस्थ और तनावमुक्त होने पर ही शरीर की सारी क्रियाएँ भली प्रकार से सम्पन्न होती हैं। इस प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योगासन अति आवश्यक है।
हमारा हृदय निरन्तर कार्य करता है। हमारे थककर आराम करने या रात को सोने के समय भी हृदय गतिशील रहता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 8000 लीटर रक्त को पम्प करता है। उसकी यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। यदि हमारी रक्त-नलिकाएँ साफ होंगी तो हृदय को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे हृदय स्वस्थ रहेगा और शरीर के अन्य भागों को शुद्ध रक्त मिल पाएगा, जिससे नीरोग व सबल हो जाएँगे। फलतः व्यक्ति की कार्य-क्षमता भी बढ़ जाएगी।
योग की उपयोगिता-मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में योग अत्यन्त उपयोगी है। शरीर, मन एवं आत्मा के बीच सन्तुलन अर्थात् योग स्थापित करना होता है। योग की प्रक्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच सन्तुलन एवं योग (जुड़ाव) स्थापित होता है, तब आत्मिक सन्तुष्टि, शान्ति एवं चेतना का अनुभव होता है। योग शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। यह शरीर के जोड़ों एवं मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शारीरिक विकृतियों को काफी हद तक ठीक करता है, शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारु करता है तथा पाचन-तन्त्र को मजबूत बनाती है। इन सबके अतिरिक्त यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्तियाँ बढ़ाता है, कई प्रकार की बीमारियों जैसे अनिद्रा, तनाव, थकान, उच्च रक्तचाप, चिन्ता इत्यादि को दूर करता है तथा शरीर को ऊर्जावान बनाता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में स्वस्थ रह पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अतः हर आयु-वर्ग के स्त्री-पुरुष के लिए योग उपयोगी है।
योग के सामान्य नियम-योगासन उचित विधि से ही करना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना रहती है। योगासन के अभ्यास से पूर्व उसके औचित्य पर भी विचार कर लेना चाहिए। बुखार से ग्रस्त तथा गम्भीर रोगियों को योगासन नहीं करना चाहिए। योगासन करने से पहले नीचे दिए सामान्य नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है-
- प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर ही योगासन का अभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद योगासन करना और भी उत्तम रहता है।
- सायंकाल खाली पेट पर ही योगासन करना चाहिए।
- योगासन के लिए शान्त, स्वच्छ तथा खुले स्थान का चयन करना चाहिए। बगीचे अथवा पार्क में योगासन करना अधिक अच्छा रहता है।
- आसन करते समय कम, हलके तथा ढीले-ढाले वस्त्र पहनने चाहिए।
- योगासन करते समय मन को प्रसन्न, एकाग्र और स्थिर रखना चाहिए। कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए।
- योगासन के अभ्यास को धीरे-धीरे ही बढ़ाएँ।
- योगासन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को हलका, शीघ्र पाचक, सात्विक और पौष्टिक भोजन करना चाहिए।
- अभ्यास के आरम्भ में सरल योगासन करने चाहिए।
- योगासन के अन्त में शिथिलासन अथवा शवासन करना चाहिए। इससे शरीर को विश्राम मिल जाता है तथा मन शान्त हो जाता है।
- योगासन करने के बाद आधे घण्टे तक न तो स्नान करना चाहिए और न ही कुछ खाना चाहिए।
योग से लाभ-छात्रों, शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए योग विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ाता है जिससे उनके लिए अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है।
पतञ्जलि के योग-सूत्र के अनुसार आसनों की संख्या 84 है। जिनमें भुजंगासन, कोणासन, पद्मासन, मयूरासन, शलभासन, धनुरासन, गोमुखासन, सिंहासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, पवर्तासन, शवासन, हलासन, शीर्षासन, धनुरासन, ताड़ासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, चतुष्कोणासन, त्रिकोणासन, मत्स्यासन, गरुड़ासन इत्यादि कुछ प्रसिद्ध आसन हैं। योग के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि और तेज बढ़ता है, अंग-प्रत्यंग में उष्ण रक्त प्रवाहित होने से स्फूर्ति आती है, मांसपेशियाँ सुदृढ़ होती हैं, पाचन शक्ति ठीक रहती है तथा शरीर स्वस्थ और हल्का प्रतीत होता है। योग के साथ मनोरंजन का समावेश होने से लाभ द्विगुणित होता है। इससे मन प्रफुल्लित रहता है और योग की थकावट भी अंनुभव नहीं होती। शरीर स्वस्थ होने से सभी इन्द्रियाँ सुचारु रूप से काम करती हैं। योग से शरीर नीरोग, मन प्रसन्न और जीवन सरस हो जाती है।
उपसंहार-आज की आवश्यकता को देखते हुए योग शिक्षा की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है। यदि आपको शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश और समाज का हित कर सकता है। अत: आज की भाग-दौड़ की जिन्दगी में खुद को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग बेहद आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में योग न सिर्फ हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण एवं मानवीय व्यस्तताओं से उपजी समस्याओं के निवारण के संदर्भ में इसकी सार्थकता और बढ़ गई है।
विज्ञापनों का हमारे जीवन पर प्रभाव
सम्बद्ध शीर्षक
- विज्ञापन की दुनिया (2016)
प्रमुख विचार-बिन्दु-
- प्रस्तावना,
- विज्ञापन का उद्देश्य,
- विज्ञापन की विशेषताएँ,
- विज्ञापन के लाभ व हानियाँ,
- पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास,
- विज्ञापन के प्रभाव,
- उपसंहार।
प्रस्तावना–“विज्ञापन समाज एवं व्यापार जगत् में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला उद्योग है, जो बदलते समय के साँचे में तेजी से ढल जाता है। ऐसा भारत में ‘ऐडगुरु’ के नाम से विख्यात प्रसून जोशी का मानना है। आज हमारे चारों ओर संचार-तन्त्र का जाल-सा बिछा हैं। एक ओर हमारे जीवन में पुस्तकें, पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र जैसे प्रिण्ट मीडिया के साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर हम घर से बाहर तक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कम्प्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अत्याधुनिक साधनों से घिरे हुए हैं, किन्तु यदि हम कहें कि मीडिया के इन सारे साधनों पर सर्वाधिक आधिपत्य विज्ञापन का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विज्ञापन न केवल इनकी आय का मुख्य स्रोत है वरन् पूरे संचार-तन्त्र का अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। तभी तो मार्शल मैकलुहन ने इसे बीसवीं सदी का सर्वोत्तम कला-विधान की संज्ञा दी है।
विज्ञापन का उद्देश्य–विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य उत्पाद को प्रभावी तरीके से आम जन तक पहुँचाना होता है। सचमुच एक छोटा-सा विज्ञापन भला क्या नहीं कर सकता! हिट हो जाए तो एक सामान्य से उत्पाद को आसमान की बुलन्दियों तक पहुँचा सकता है। विज्ञापन की बानगी देखिए-“दो बूंद जिन्दगी की’ (पोलियो उन्मूलन), ‘जागो रे’ (टाटा चाय), ‘दाग अच्छे हैं’ (सर्फ एक्सेल) अथवा ‘नो उल्लू बनाईंग’ (आइडिया मोबाइल) जैसे विज्ञापन इतने प्रचलित हुए कि सहज ही लोगों की जुबान पर चढ़ गए। यद्यपि रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के छोटे-से समय अथवा समाचार-पत्रों के छोटे से हिस्से के द्वारा विज्ञापनों को अपना उद्देश्य पूरा करना पड़ता है, फिर भी इनमें रचनात्मकता देखते ही बनती है। इसमें दो राय नहीं है कि मैगी, साबुन, शैम्पू, मोबाइल जैसे उत्पादों में वृद्धि का कारण इनके रचनात्मक विज्ञापन ही हैं और वर्तमान समय का सच भी यही है कि आज किसी भी उत्पाद के प्रचार-प्रसार का सबसे प्रभावशाली माध्यम विज्ञापन ही है।
प्रसून जोशी के शब्दों में-“विज्ञापन का क्षेत्र अति सृजनात्मक है। मैं विज्ञापन लिखने के दौरान तुकबन्दी न कर पूरी कविता की रचना करता हूँ; जैसे-उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा अथवा हाँ मैं क्रेजी हूँ! एक अच्छा विज्ञापन लोगों के दिल में उतर जाता है और वे ब्राण्ड से जुड़ जाते हैं।”
विज्ञापन, उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण से निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर विचारों, उत्पादों एवं सेवाओं से सम्बन्धित सन्देशों का अव्यक्तिगत संचार है। यह मुद्रित, ऑडियो अथवा वीडियो रूप में हो सकता है। इसके प्रसारण के लिए समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों को माध्यम बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स इत्यादि का प्रयोग भी विज्ञापन के लिए किया जाता है। जूते-चप्पल से लेकर लिपस्टिक, पाउडर एवं दूध-दही यानी दुनिया की ऐसी कौन-सी चीज है, जिसका विज्ञापन किसी-न-किसी रूप में कहीं प्रकाशित न होता हो! यहाँ तक कि विवाह के लिए वर या वधू की तलाश हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित होते हैं।
विज्ञापन की विशेषताएँ-विज्ञापन की विशेषताओं पर गौर करें, तो पता चलता है कि ये सन्देश के अव्यक्तिगत संचार होते हैं। इनका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का संवर्द्धन करना होता है। इनके प्रायोजक द्वारा लोगों को वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला एक सन्देश प्रेषित किया जाता है। इस तरह, विज्ञापन संचार का भुगतान किया हुआ एक रूप है।
विज्ञापन से कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह उत्पादों, मूल्यों, गुणवत्ता, बिक्री सम्बन्धी जानकारियों, विक्रय उपरान्त सेवाओं इत्यादि के बारे में उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। यह नए उत्पादों के प्रस्तुतीकरण, वर्तमान उत्पादों के उपभोक्ताओं को बनाए रखने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी बिक्री बढ़ाने में निर्माताओं की मदद करता है। यह लोगों को अधिक सुविधा, आराम, बेहतर जीवन-पद्धति उपलब्ध कराने में सहायक होता है।
इन सबके अतिरिक्त, विज्ञापन समाचार-पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन की आय का प्रमुख स्रोत होता है। यदि सही मात्रा में इन माध्यमों को विज्ञापन न मिलें, तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो समाचार-पत्र हम दो या तीन रुपये में खरीदते हैं, उसकी छपाई का ही व्यय दस रुपये से अधिक होता है। फिर प्रश्न उठता है कि हमें कम कीमत पर यह कैसे उपलब्ध हो जाता है। दरअसल, विज्ञापनों से प्राप्त आय से इसकी भरपाई की जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि यदि संचार माध्यमों को पर्याप्त विज्ञापन न मिलें, तो इनके बन्द होने का खतरा हो सकता है। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ही आज खेल-कूद आयोजनों एवं कार्यक्रमों को प्रायोजित करती हैं। टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो या रेडियो पर ऑखों देखा हाल, इन सबको बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ही प्रसारित करती हैं और इसका उद्देश्य होता है—उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं का विज्ञापन। इस तरह, विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन भी होता है। आजकल टेलीविजन पर अत्यधिक मात्रा में प्रसारित विज्ञापनों के कारण लोगों को इससे अरुचि होने लगी है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि यदि विज्ञापन न हों, तो किसी कार्यक्रम का प्रसारण भी नहीं हो पाएगा। इस तरह देखा जाए, तो विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन हो पाता है। खिलाड़ियों के लिए विज्ञापन कुबेर का खजाना बन चुके हैं।
आजकल तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विज्ञापन संचार के सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं। समाचार-पत्र एवं रेडियो, टेलीविज़न ही नहीं, इण्टरनेट पर भी आजकल विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा जा सकता है। सरकार की विकासोन्मुखी योजनाएँ-साक्षरता अभियान, परिवार नियोजन, महिला सशक्तीकरण, कृषि एवं विज्ञान सम्बन्धी योजनाएँ, पोलियो एवं कुष्ठ निवारण अभियान इत्यादि विज्ञापन के माध्यम से ही त्वरित ति से क्रियान्वित होकर प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। इस तरह से विज्ञापन समाजसेवा में भी सहायक होता है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन एवं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय द्वारा ‘पोलियो मुक्त अभियान के लिए प्रस्तुत किया गया विज्ञापन ‘दो बूंद जिन्दगी की’ इसका जीता-जागता उदाहरण है। इस विज्ञापन का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
केवल व्यावसायिक लाभों के लिए कम्पनियों द्वारा ही विज्ञापनों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जाता। अब राजनीतिक दल भी अपने विचारों एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। इस तरह, चुनावों के समय लोकमत के निर्माण में भी विज्ञापनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। बिल बर्नबेक के अनुसार, विज्ञापन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्त्व सच है।
विज्ञापन के लाभ व हानियाँ-विज्ञापन से यदि कई लाभ हैं, तो इससे हानियाँ भी कम नहीं हैं। विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर ठण्डे पेय पदार्थों को ही लीजिए। जो ठण्डा पेय पदार्थ बाजार में दस रुपये में उपलब्ध होता है, उसका लागत मूल्य मुश्किल से 5 से 7 रुपये के आस-पास होता है, किन्तु इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं। इसलिए इनकी कीमत में अनावश्यक वृद्धि होती है।
कभी-कभी विज्ञापन हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को भी क्षति पहुँचाता है। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास में विज्ञापनों का भी हाथ है। ‘वैलेण्टाइन डे’ हो यो ‘न्यू ईयर ईव’ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इनका लाभ उठाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। इण्टरनेट से लेकर गली-मुहल्ले तक में इनसे सम्बन्धित सामानों को बाजार लग जाता है। इस तरह कम्पनियों को करोड़ों को लाभ होता है तथा ग्राहकों को भी उचित मूल्य पर वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं।
पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास–विज्ञापन से होने वाली एक और हानि यह है कि विज्ञापनदाताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भण्डाफोड़ करने से जनसंचार माध्यम बचते हैं। विज्ञापनों से होने वाले आर्थिक लाभ के कारण धन लेकर समाचार प्रकाशित करने की प्रवृत्ति भी आजकल बढ़ रही है। इससे पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास हुआ है। मीडिया को लोकतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाता है। विज्ञापनदाताओं के अनुचित प्रभाव एवं व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता देने के कारण मीडिया के उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि सरकारी विज्ञापनों के लोभ में समाचार-पत्र एवं टीवी चैनल सरकार के विरोध में कुछ प्रकाशित या प्रसारित नहीं करते।।
विज्ञापन से एकाधिकार की प्रवृत्ति का भी सृजन होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रारम्भ से ही यह प्रयास करती रही है कि कम्प्यूटर की दुनिया में उसका एकाधिकार रहे। इसके लिए वह समस-समय पर विज्ञापनों का सहारा लेती है। विज्ञापनों के माध्यम से एकाधिकार की लड़ाई का सबसे अच्छा उदाहरण कोकाकोला एवं पेप्सी कम्पनियों के बीच विज्ञापनों की होड़ है। यह हमेशा माँग में वृद्धि करवाने में सहायक होता है।
विज्ञापन के प्रभाव-लुभावने विज्ञापनों द्वारा हमारी सोच को बीमार कर दिया जाता है और हम उनकी ओर स्वयं को बँधे हुए पाते हैं। आज मुँह धोने के लिए हजारों किस्म के साबुन और फेशवास तथा मुख की कांति को बनाए रखने के लिए हजारों प्रकार की क्रीम मिल जाएँगे, जिनमें विज्ञापनों द्वारा हमें यह विश्वास दिला दिया जाता है कि यह क्रीम हमें जवान और सुंदर बना देगा। रंग यदि काला है तो वह गोरा हो जाएगा। इन विज्ञापनों में सत्यता लाने के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ियों और फिल्मी कलाकारों को लिया जाता है। हम इन कलाकारों की बातों को सच मानकर अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं परन्तु नतीजा कुछ भी सच नहीं निकलता।
हमें विज्ञापन देखकर जानकारी अवश्य लेनी चाहिए परन्तु विज्ञापनों को देखकर वस्तुएँ नहीं लेनी चाहिए। विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है, वह शत-प्रतिशत सही नहीं होता। विज्ञापन हमारी सहायता करते हैं कि बाजार में किस प्रकार की सामग्री आ गई है। हमें विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विज्ञापन ग्राहक और निर्माता के बीच कड़ी का काम करते हैं।
ग्राहकों को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए विज्ञापनों द्वारा आकर्षित किया जाता है। लेकिन इनके प्रयोग करने पर ही हमें उत्पादों की गुणवत्ता का सही पता चलता है। आज आप कितने ही ऐसे साबुन, क्रीम और पाउडरों के विज्ञापनों को देखते होंगे जिनमें यह दावा किया जाता है कि यह साँवले रंग को गोरा बना देता है, परन्तु ऐसा नहीं होता है। लोग अपने पैसे व्यर्थ में बरबाद कर देते हैं। उनके हाथ मायूसी ही लगती है। हमें चाहिए कि सोच-समझकर उत्पादों का प्रयोग करें। विज्ञापन हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं परन्तु कौन-सा उत्पाद हमारे काम का है या नहीं यह हमें तय करना चाहिए।
उपसंहार-विज्ञापन की दुनिया एक रोचक दुनिया है। जहाँ जैसा है, ग्लैमर है, शोहरत है एवं सफलता की ऊँचाइयाँ हैं। कई मॉडलों के प्रसिद्ध होने में विज्ञापनों का योगदान रहा है। कई फिल्मों के हिट होने के पीछे भी विज्ञापन की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। विज्ञापन की दुनिया की सबसे खास बात इसकी रचनात्मकता होती है। कुछ विज्ञापन तो हास्य-व्यंग्य से भी भरपूर होते हैं, जिसके कारण इनसे भी लोगों का अच्छा मनोरंजन हो जाता है। नि:सन्देह जानकारी बढ़ाने, मेल-मिलाप करने जैसे सकारात्मक साधन के रूप में कार्य करने पर विज्ञापन जनकल्याण के साथ-साथ देशहित में भी सहायक होगा। नॉर्मन डगलस से कहा भी है-“आप अपने विज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्र के आदर्शों को प्रकट कर सकते हैं।’
We hope the UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्य, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.