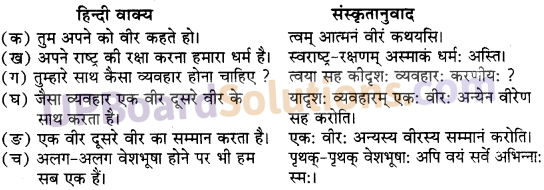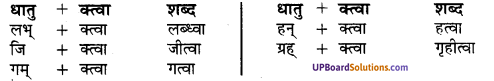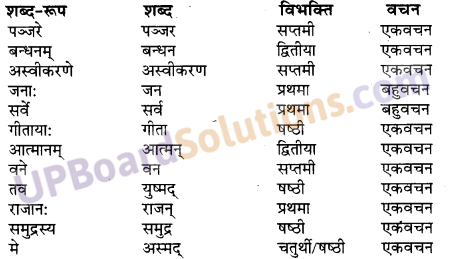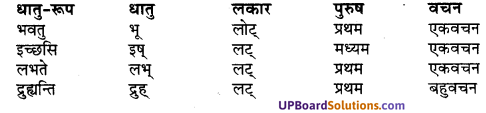UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 आपदाएँ (अनुभाग – तीन)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Social Science. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 आपदाएँ (अनुभाग – तीन).
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है? किसी एक प्राकृतिक आपदा पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
या
आपदा से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो आपदाओं का वर्णन कीजिए। [2013]
या
प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? किन्हीं चार प्राकृतिक आपदाओं के विषय में लिखिए। [2015]
उत्तर :
प्राकृतिक आपदा
प्राकृतिक कारणों से या प्रकृति (Nature) के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है; जैसे-भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा, समुद्री लहरें, भूस्खलन, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान आदि। (UPBoardSolutions.com) दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक रूप से घटित वे समस्त घटनाएँ जो प्रलयंकारी रूप ग्रहण कर सामान्य मानव सहित सम्पूर्ण मानवजगत् के लिए विनाश का दृश्य उपस्थित कर देती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ कहलाती हैं। इन आपदाओं का सीधा सम्बन्ध प्रकृति या पर्यावरण से होता है।

भूस्खलन
भूमि के एक सम्पूर्ण भाग अथवा उसके विखण्डित एवं विच्छेदित खण्डों के रूप में खिसक जाने अथवा गिर जाने को. भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन संसार में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख हैं, भूस्खलन एक व्यापक प्राकृतिक आपदा है, जिससे बारह महीने जान और माल का नुकसान होता है। यह भूस्खलन परिवहन तथा संचार-व्यवस्था को भी बाधित करता है तथा रिहायशी बस्तियों को भी नष्ट करता है। भू-क्षरण (Land erosion) तथा भूस्खलन (Land slide) अलग-अलग प्राकृतिक घटनाएँ हैं, जिनको भूलवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर लिया जाता है। भू-क्षरण में धरातल की मिट्टी किसी भी प्रक्रम के द्वारा अपने स्थान से अन्यत्र बह जाती है; जब कि भूस्खलन में भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े टूटकर सड़कों व बस्तियों को मलबे के नीचे दबा देते हैं, कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर देते हैं तथा नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं।
कारण
भूस्खलन का प्रमुख कारण पर्वतीय ढालों की चट्टानों का कमजोर होना है। चट्टानों के कमजोर होने पर उनमें घुसा हुआ पानी चट्टानों की बँधी हुई मिट्टी को ढीला कर देता है। यही ढीली हुई मिट्टी ढाल की ओर भारी ” दबाव डालती है। फलतः नीचे की सूखी चट्टानें ऊपर के भारी और गीले मलबे एवं चट्टानों का भार नहीं सँभाल पातीं, इसलिए वे नीचे की ओर खिसक जाती हैं और भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ी ढालों और चट्टानों के कमजोर पड़ने के प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण हो सकते हैं। भूस्खलन की उत्पत्ति या कारणों को निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है
- भूस्खलन भूकम्पों या अचानक शैलों के खिसकने के कारण होते हैं।
- खुदाई या नदी-अपरदन के परिणामस्वरूप ढाल के आधार की ओर भी तेज भूस्खलन हो जाते हैं।
- भारी वर्षा या हिमपात के दौरान पर्वतों की तेज ढालों पर चट्टानों का बहुत बड़ा भाग जल तत्त्व की अधिकता एवं आधार के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असन्तुलित होकर अचानक तेजी के साथ विखण्डित होकर गिर जाता है। अत: चट्टानों पर दबाव की वृद्धि भूस्खलन का मुख्य कारण. होती है।
- भूस्खलन का कारण त्वरित भूकम्प, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, (UPBoardSolutions.com) अनियमित वन कटाई आदि भी होता है।
- सड़क एवं भवन बनाने के लिए प्राकृतिक ढलानों को सपाट स्थिति में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भी पहाड़ी ढालों पर भूस्खलन होने लगते हैं। वास्तव में मुलायम वे कमजोर पारगम्य चट्टानों में रिसकर जमा हुए हिम या जल का बोझ ही पर्वतीय ढालों पर चट्टानों के टूटने और खिसकने का प्रमुख कारण है।

निवारण
भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है फिर भी मानवे-क्रियाएँ इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके न्यूनीकरण की मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित हैं
- भूमि उपयोग–वनस्पतिविहीन ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। अत: ऐसे स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनस्पति उगाई जानी चाहिए। भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों के द्वारा सुझाये गये उपायों को अपनाकर, भूमि के उपयोग तथा स्थल की जाँच से ढलान को स्थिर बनाने वाली विधियों को अपनाकर भूस्खलन से होने वाली हानि को 95% से अधिक कम किया जा सकता है। जल के प्राकृतिक प्रवाह में कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए।
- प्रतिधारण दीवारें भूस्खलन को सीमित करने तथा मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सड़कों के किनारों पर प्रतिधारण दीवारें तीव्र ढाल पर बनायी जानी चाहिए जिससे ऊँचे पर्वत से पत्थर सड़क पर गिर न जाएँ। रेल लाइनों के लिए प्रयोग की जाने वाली सुरंगों के पश्चात् काफी दूर तक प्रतिधारण दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- स्थानीय जल-प्रवाह नियन्त्रण-वर्षा के जल तथा चश्मों से जल-प्रवाह के कारण घटित भूस्खलनों को नियन्त्रित करने के लिए स्थलीय जल-प्रवाह को नियन्त्रित करना चाहिए, जिससे भूस्खलन हेतु पानी भूमि में प्रवेश न कर सके।
- पर्वतीय ढलानों को स्थिर करना–पर्वतीय ढलानों को स्थिर करके भी भूस्खलन से होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है। ढलानों को घास उगाकर, पौधों का रोपण करके एवं वृक्ष लगाकर स्थिर एवं मजबूत किया जा सकता है। अधिक तीव्र ढाल वाले स्थानों पर जब तक पर्याप्त वानस्पतिक आवरण विकसित न हो जाए, तब तक मिट्टी को अस्थायी रूप से रोकने के लिए टाट, नारियल जटा आदि का (UPBoardSolutions.com) उपयोग किया जा सकता है।
- भवनों के समीप अवरोधक बनाना–खड़ी या तीव्र ढाल पर बने भवनों के निकट ऐसे अवरोधकों का निर्माण करना चाहिए, जो छोटे-छोटे भूस्खलनों को रोकने में समर्थ हों; अर्थात् इनका निर्माण ऐसा होना चाहिए, जिससे ये भूस्खलन के समय गिरने वाले मलबे की गति के सामने टिक सकें। अवरोधकों के निर्माण के समय पानी की निकासी की पूर्ण व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए।
- अभियान्त्रिकी संरचना-भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत नींव वाले भवंने तथा अन्य अभियान्त्रिकी संरचनाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए। भूमिगत संयन्त्रों को तकनीकी रूप से ऐसे निर्मित किया जाना चाहिए कि वे भूस्खलन से क्षतिग्रस्त न हों। इनके समीप भी प्रतिधारण दीवारें बनायी जानी चाहिए। इनके निर्माण के समय भी पानी के निकास का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।
- वनस्पति आवरण में वृद्धि–वनस्पति आवरण में वृद्धि भूस्खलन को नियन्त्रित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली, सस्ता तथा उपयोगी रास्ता है। यह मिट्टी की ऊपरी सतह को निचली सतह से बाँधे रखता है तथा स्थलीय जल-प्रवाह को धीमा कर मृदा के अपरदन को रोकता है।
- भूस्खलन सम्भावित एवं प्रभावित क्षेत्र की पहचान कर उन्हें मानचित्रित किया जाना चाहिए। इसका प्रभावित वर्ग में प्रचार-प्रसार भी आवश्यक है, जिससे वह सचेत हो सके। भारत में भूस्खलन के प्रमुख क्षेत्र हैं-
- हिमालय,
- उत्तर-पूर्वी पर्वतीय भाग,
- पश्चिमी घाट तथा नीलगिरि,
- पूर्वी घाट एवं
- विन्ध्याचल। उपर्युक्त निवारक-प्रबन्धक उपायों को अपनाकर भूस्खलन रूपी आपदा से होने वाली हानि को भी न्यूनतम किया जा सकेगा।

[ संकेत–अन्य आपदाओं के लिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न संख्या 2, 4 व 6 देखें।]
प्रश्न 2.
भूकम्प के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा इससे भवन-सम्पत्ति की रक्षा कैसे करेंगे ? लिखिए।
उत्तर :
प्राकृतिक आपदाओं में भूकम्प सबसे अधिक विनाशकारी, भयानक एवं प्रभावकारी आपदा है। इसके कारण अनगिनत लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और धन-सम्पत्ति को भी व्यापक क्षति पहुँचती है। भूकम्प भूतल की आन्तरिक (UPBoardSolutions.com) शक्तियों में से एक है। ऐसे तो भूगर्भ में प्रतिदिन कम्पन होते रहते हैं, लेकिन जब ये कम्पन अत्यधिक तीव्र होते हैं तो भूकम्प कहलाते हैं। साधारणतया भूकम्प एक आकस्मिक घटना है, जो भू-पटल में हलचल पैदा कर देती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी अनायास ही वेग से काँपने लगती है। इसे ही भूचाल या भूकम्प कहते हैं। यह एक विनाशकारी घटना है।

कारण
भूगर्भशास्त्रियों ने भूकम्प के निम्नलिखित प्रमुख कारण बताये हैं।
1. ज्वालामुखीय उद्गार- जब विवर्तनिक हलचलों के कारण भूगर्भ में विद्यमान गैसयुक्त द्रवित लावा भू-पटल की ओर प्रवाहित होता है तो उसके दबाव से भू-पटल की शैलें हिल उठती हैं। यदि लावा के मार्ग में कोई भारी चट्टान आ जाए तो प्रवाहशील लावा उस चट्टान को वेग से धकेलता है, जिससे भूकम्प आ जाता है।
2. भू-असन्तुलन में अव्यवस्था- भू-पटल पर विभिन्न बल समतल समायोजन में लगे रहते हैं, जिससे भूगर्भ की सियाल एवं सिमा की परतों में परिवर्तन होते रहते हैं। यदि ये परिवर्तन एकाएक तथा तीव्र गति से हो जाये तो पृथ्वी में कम्पन प्रारम्भ हो जाता है।

3. जलीय भार- मानव द्वारा निर्मित जलाशय, झील अथवा तालाब के धरातल के नीचे की चट्टानों पर भार एवं दबाव के कारण अचानक परिवर्तन हो जाते हैं तथा इनके कारण ही भूकम्प आ जाता है।
4. भू-पटल में सिकुड़न- विकिरण के माध्यम से भूगर्भ की गर्मी धीरे-धीरे कम होती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी में सिकुड़न आती है। यह सिकुड़न पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देती है। जब यह प्रक्रिया तीव्रता (UPBoardSolutions.com) से होती है, तो भू-पटल पर कम्पन प्रारम्भ हो जाते हैं।
5. प्लेट विवर्तनिकी– महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन विशालकाय दृढ़ भू-खण्डों से बने हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। सभी प्लेटें विभिन्न गति से सरकती रहती हैं। कभी-कभी जब दो प्लेटें परस्पर टकराती हैं, तब भूकम्प आते हैं।
6. संसाधनों का अत्यधिक दोहन- पृथ्वी से जल, खनिज तेल व गैस का अत्यधिक दोहन करने के कारण जब सतह के भीतर स्थान खाली हो जाता है, तब उसे भरने व सन्तुलित करने के लिए भूमि में हलचल उत्पन्न होती है, जिससे भूकम्प आते हैं।
भवन-सम्पत्ति की रक्षा के उपाय
भारत में अब तक आये भूकम्पों से सबसे अधिक हानि असुरक्षित भवनों के निर्माण से हुई है। इसका कारण यह है कि भवनों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को बिना किसी तकनीक के प्रयोग किया जाता है, जो भूकम्प के समय गिरकर अत्यधिक धन-जन की हानि करते हैं। अत: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित भवनों के निर्माण हेतु निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए

1. भवनों की आकृति- भवन का नक्शा साधारणतया आयताकार होना चाहिए। लम्बी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट-पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। जहाँ तक हो सके T, L, U और X-आकार के नक्शों वाले बड़े भवनों को (UPBoardSolutions.com) उपयुक्त स्थानों पर अलग-अलग खण्डों में बाँटकर आयताकार खण्ड बना लेना चाहिए। खण्डों के बीच खास अन्तर से चौड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए, जिससे भूकम्प के समय भवन हिल-डुल सके और क्षति न हो।
2. नींव– जहाँ आधार भूमि में विभिन्न प्रकार की अथवा नरम मिट्टी हो वहाँ नींव में भवन के कॉलमों को भिन्न-भिन्न व्यवस्था में स्थापित करना चाहिए। ठण्डे देशों में मिट्टी में आधार की गहराई जमाव-बिन्दु क्षेत्र के पर्याप्त नीचे तक होनी चाहिए, जब कि चिकनी मिट्टी में यह गहराई दरार के सिकुड़ने के स्तर से नीचे तक होनी चाहिए। ठोस मिट्टी वाली परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के आधार का प्रयोग कर सकते हैं। चूने या सीमेण्ट व कंक्रीट से बनी ठोस और उचित चौड़ाई वाली नींव पर भवनों के आधार का निर्माण करना उचित रहता है।
3. दीवारों में खुले स्थान– दीकारों में दरवाजों और खिड़कियों की बहुलता के कारण, उनकी भार-रोधक क्षमता कम हो जाती है। अतः ये कम संख्या में तथा दीवारों के बीचों-बीच स्थित होने | चाहिए। किनारों पर बनाये गये खुले स्थानों से दीवार के गिरने की अधिक सम्भावना होती है।
4. कंक्रीट से बने बैण्डों का प्रयोग- भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में, दीवारों को मजबूती प्रदान करने तथा उनकी कमजोर जगहों पर समतल रूप से मुड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कंक्रीट के मजबूत बैण्ड बनाये जाने चाहिए जो स्थिर विभाजक दीवारों सहित सभी बाह्य तथा आन्तरिक दीवारों पर लगातार काम करते रहते हैं। इन बैण्डों में प्लिन्थ, लिण्टल, रूफ, ईव, फ्लोर, वर्टिकल, रैफ्टर, होल्डिग डाउन, गेबल आदि बैंड सम्मिलित हैं।

5. वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट- दीवारों के कोनों और जोड़ों में वर्टिकल स्टील लगाया जाना चाहिए, जो सभी मंजिलों और फर्श वाले बैण्ड से गुजरता हो। भूकम्पीय क्षेत्रों, खिड़कियों तथा दरवाजों की चौखट में भी वर्टिकल रीइन्फोर्समेंट की व्यवस्था (UPBoardSolutions.com) की जानी चाहिए। वस्तुत: कोई भी भवन भूकम्प से पूर्णतया सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन भूकम्प प्रतिरोधी अवश्य हो सकता है; यदि भवन की निर्माण योजना के बुनियादी सिद्धान्तों-हलकापन, निर्माण की निरन्तरता, आकार, द्रव्यमान आदि का ध्यान रखा जाए।
प्रश्न 3.
बाढ़ आपदा निवारण हेतु प्रमुख उपाय लिखिए। या बाढ़ नियन्त्रण हेतु कोई दो उपाय सुझाइए। [2013]
या
बाढ़ आपदा की समस्या के समाधान के लिए चार सुझाव दीजिए। [2018]
उत्तर :
बाढ़ आपदा निवारण हेतु प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं
1. सीधा जलमार्ग– बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में जलमार्ग को सीधा रखना चाहिए जिससे वह तेजी से एक सीमित मार्ग से बह सके। टेढ़ी-मेढ़ी धाराओं में बाढ़ की सम्भावना अधिक होती है।
2. जलमार्ग-परिवर्तन– बाढ़ के उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहाँ प्राय: बाढ़े आती हैं। ऐसे स्थानों से जलमार्ग को मोड़ने के लिए कृत्रिम ढाँचे बनाये जाते हैं। यह कार्य वहाँ किया जाता है जहाँ कोई बड़ा जोखिम न हो।
3. कृत्रिम जलाशयों का निर्माण- वर्षा के जल से आबादी-क्षेत्र को बचाने के लिए कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन जलाशयों में भण्डारित जल को बाद में सिंचाई अथवा पीने के लिए। प्रयोग किया जा सकता है। इन जलाशयों में बाढ़ के जल को मोड़ने के लिए जल कपाट लगे होते हैं।
4. बाँध-निर्माण- आबादी वाले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए तथा जल के प्रवाह को उस ओर से रोकने के लिए रेत के थैलों का बाँध बनाया जा सकता है।
5. कच्चे तालाबों का निर्माण- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कच्चे तालाबों (UPBoardSolutions.com) का अधिक-से-अधिक निर्माण कराया जाना चाहिए। ये तालाब वर्षा के जल को संचित कर सकते हैं, जिनका जल आवश्यकता के समय उपयोग में भी लाया जा सकता है।

6. नदियों को आपस में जोड़ना- विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सकता है। अधिक जल वाली नदियों का जल कम जल वाली नदियों में चले जाने से भी बाढ़ की स्थिति से सुरक्षा हो सकती है।
7, बस्तियों का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण– बस्तियों का निर्माण नदियों के मार्ग से हटकर किया जाना चाहिए। नदियों के आस-पास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सुरक्षा के लिए मकान ऊँचे चबूतरों पर बनाये जाने चाहिए तथा इनकी नींव व चारों ओर की दीवारों को मजबूत बनाना चाहिए।
8. तटबन्धों का निर्माण नदियों पर तटबन्धों का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे किसी अन्य क्षेत्र में बाढ़ की समस्या न उत्पन्न हो। तटबन्धों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि नदियों का जल ऊँचा होने पर ये तटबन्ध टूट सकते हैं तथा अधिक विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। उपर्युक्त निवारक उपायों के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु विस्फोटकों के प्रयोग को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे भूस्खलन की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। ढालयुक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण तथा वन-विनाश को रोकने का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए।

प्रश्न 4.
‘सूखा क्या है ? इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर :
सूखा’ वह स्थिति है जिसमें किसी स्थान पर अपेक्षित तथा सामान्य वर्षा से भी कम वर्षा होती है और यह स्थिति एक लम्बी अवधि तक रहती है। सूखा उस समय भयंकर रूप धारण कर लेता है जब इसके साथ-साथ ताप भी आक्रमण करता है। शुष्क तथा (UPBoardSolutions.com) अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में सूखी एक सामान्य समस्या है, किन्तु पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं हैं। मानसूनी वर्षा के क्षेत्र सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सूखा एक मौसम सम्बन्धी आपदा है तथा किसी अन्य विपत्ति की अपेक्षा अधिक धीमी गति से आता है।
कारण
वस्तुतः सूखी एक प्राकृतिक आपदा है, परन्तु वर्तमान समय में प्रकृति तथा मानव दोनों ही इसके मूल में हैं। सूखा के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं
1. अत्यधिक चराई तथा जंगलों की कटाई- अत्यधिक चराई तथा जंगलों की कटाई के कारण हरियाली की पट्टी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्षा कम मात्रा में होती है और यदि होती भी है तो जल भूतल पर तेजी से बह जाता है। इसके कारण मिट्टी का कटाव होता है तथा सतह से नीचे का जल-स्तर कम हो जाता है।
2. ग्लोबल वार्मिंग- ग्लोबल वार्मिंग वर्षा की प्रवृत्ति में बदलाव का कारण बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप वर्षा वाले क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाते हैं।
3. कृषि योग्य समस्त भूमि का उपयोग– बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य-सामग्री उगाने हेतु लगभग समस्त कृषि योग्य भूमि पर जुताई व खेती की जाने लगी है। इसके परिणामस्वरूप मृदा की उर्वरा-शक्ति क्षीण होती जा रही है तथा वह रेगिस्तान में परिवर्तित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्षा की थोड़ी कमी भी सूखे का कारण बन जाती है।
4. वर्षा का असमान वितरण- देश में वर्षा का असमान वितरण दोनों ही तरीके से व्याप्त है। विभिन्न स्थानों पर न तो वर्षा की मात्रा समान है और न ही अवधि। हमारे देश में कुल जोती जाने वाली भूमि का लगभग 70% भाग सूखा सम्भावित क्षेत्र है। (UPBoardSolutions.com) इस क्षेत्र में यदि कुछ वर्षों तक लगातार वर्षा न हो तो सूखे की अत्यन्त दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है।
5. जलचक्र- वर्षा जलचक्र के नियमित संचरण, प्रवाह एवं प्रक्रिया का परिणाम है, किन्तु जब कभी जलचक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो वर्षा के अभाव के कारण सूखे की स्थिति आ जाती है। आधुनिक विकास ने जलचक्र की प्राकृतिक प्रक्रिया की कड़ियों को तोड़ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

6. भूमिगत जल का अधिक दोहन- भूमिगत जलस्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भी देश के कई प्रदेशों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सूखे का कारण वर्षा की कमी को माना जाता है। किन्तु मात्र वर्षा कम होने या न होने से ही सूखा नहीं होता। जब भूमिगत जल निकासी की दर भूमि में जाने वाले जल की दर से अधिक हो जाती है तो वर्षा न होने की स्थिति में सूखा पड़ जाता है।
7. नदी मार्गों में परिवर्तन- सततवाहिनी नदियाँ केवल सतही जल का बहाव मात्र नहीं होतीं अपितु ये नदियाँ भूमिगत जलस्रोतों को भी जल प्रदान करती हैं। नदी का मार्ग बदल जाने पर निकटवर्ती भूमिगत जलस्रोत सूखने लगते हैं।
8. खनन कार्य- देश के अनेक भागों में अवैज्ञानिक ढंग से किया गया खनन कार्य भी सूखा संकट का . प्रभावी कारण होता है। हिमालय की तराई एवं दून घाटी के क्षेत्रों में, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेमी से अधिक रहती है, अनियोजित खनन कार्यों के कारण अनेक प्राकृतिक जलस्रोत सूख गये
9. मिट्टी का संगठन– मिट्टी जैविक संगठन द्वारा बना प्रकृति का महत्त्वपूर्ण पदार्थ है, जो स्वयं जल एवं नमी का भण्डार होता है। वर्तमान समय में मिट्टी का संगठन असन्तुलित हो गया है, इसलिए मिट्टी की जलधारण क्षमता अत्यन्त कम हो गयी है। जैविक (UPBoardSolutions.com) पदार्थ (वनस्पति आदि) मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। वर्तमान समय में भूमि-क्षरण के कारण मिट्टी का वनस्पतीय आवरण कम हो गया है। इसलिए जलधारण क्षमता के अभाव के कारण सूखे का सामना अधिक करना पड़ता है।
प्रश्न 5.
ओजोन-क्षरण के कारण, प्रभाव एवं नियन्त्रण पर लेख लिखिए। या ओजोन-क्षरण को रोकने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। [2013]
उत्तर:
ओजोन ऑक्सीजन तत्त्व का ही एक रूप है। समतापमण्डल में सूर्य की पराबैंगनी किरणें वायुमण्डलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन गैस बनाती हैं।
ओजोन गैस का महत्त्व
वायुमण्डल में ओजोन गैस की उपस्थिति पर्यावरण के जैविक तत्त्वों के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। सूर्य से आने वाले विकिरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणों का 99% से भी अधिक भाग इस गैस के द्वारा वायुमण्डल में प्रवेश के साथ ही अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषण से पृथ्वी पर जीवन के विविध रूप, पराबैंगनी किरणों के कई हानिकारक प्रभावों से बच पाते हैं। ओजोन गैस उष्मा उत्पन्न करने वाली लाल अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है जिससे पृथ्वी का तापमान सन्तुलित रहता है।
ओजोन गैस के क्षरण के कारण
वायुमण्डल में ओजोन गैस की मात्रा 0.5% प्रतिवर्ष के हिसाब से कम हो रही है तथा अण्टार्कटिका के ऊपर स्थित वायुमण्डल में 20 से 30% तक ओजोन की मात्रा कम हो गयी है। इसके अतिरिक्त, ओजोन की कमी वाले छोटे-छोटे छिद्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, चिली, अर्जेण्टीना आदि स्थानों पर देखे गये हैं। ओजोन में हो रही कमी का कारण रासायनिक अभिक्रियाओं को माना जाता है जो ओजोन को ऑक्सीजन में (UPBoardSolutions.com) परिवर्तित कर रही हैं। ओजोन गैस में विघटन उत्पन्न करने वाला प्रमुख रसायन क्लोरो-फ्लोरो कार्बन यौगिक है। इस यौगिक का उपयोग शीतलीकरण उद्योग (रेफ्रीजरेटर्स, एयर-कण्डीशनर), अग्निरोधी पदार्थों, प्लास्टिक, रंग और एरोजोल उद्योग में होता है। क्लोरो-फ्लोरो कार्बन से मुक्त हुआ क्लोरीन का एक परमाणु, ओजोन के एक लाख अणुओं को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। इसी तरह धीरे-धीरे ओजोन परत का क्षरण होता है।

ओजोन क्षरण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फलतः ‘हिस्टेमिन’ नामक रसायन के निकल जाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप, ‘मिलिग्रेण्ड’ नामक त्वचा कैंसर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अल्सर आदि रोग हो जाते हैं। पराबैंगनी किरणों का प्रभाव आँखों के लिए अत्यन्त घातक होता है। आँखों में सूजन तथा घाव होना तथा मोतियाबिन्द जैसी बिमारियों में वृद्धि का कारण भी इन किरणों का पृथ्वी की सतह पर आना है।
ओजोन क्षरण को रोकने के उपाय
ओजोन गैस के क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए
1. प्रदूषण पर नियन्त्रण– प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें वायुमण्डल में फैलती हैं। जिनका ओजोन परत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
2. CFC गैसों पर नियन्त्रण– फैक्ट्रियों, रसायन उद्योगों आदि से निकलने वाली क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, ओजोन के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। प्रशीतन तथा वातानुकूलित मशीनों द्वारा इन गैसों का विस्तार बढ़ता है।
3. नाइट्रस ऑक्साइड- नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हानिकारक (UPBoardSolutions.com) गैसें जो जेट विमानों द्वारा ऊपरी वायुमण्डल में फैलती हैं, उन्हें नियन्त्रित किया जाना चाहिए।
4. वृक्षारोपण- वृक्षारोपण द्वारा प्रदूषण रोका जा सकता है।

प्रश्न 6.
‘सूनामी’ से क्या अभिप्राय है ? इसके कारणों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
समुद्री लहरें (सूनामी)
समुद्री लहरें कभी-कभी अत्यधिक विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। इनकी ऊँचाई, 15 मीटर और कभी-कभी इससे भी अधिक होती है। ये तट के आस-पास की बस्तियों को पूर्णरूपेण तबाह कर देती हैं। इनकी रफ्तार समुद्र की गहराई के साथ-साथ बढ़ती जाती है, जब कि उथले सागर में इनकी रफ्तार कम होती है। ये लहरें मिनटों में ही तट तक पहुँच जाती हैं। जब ये लहरें उथले पानी में प्रवेश करती हैं, तो इनकी रफ्तार कम (UPBoardSolutions.com) हो जाती है परन्तु पीछे से आती और लहरें एक के ऊपर एक होकर, लहरों की ऊँची दीवार बना देती हैं और भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर कई मीटर ऊपर तक उठती हैं। तटवर्ती मैदानी इलाकों में इनकी रफ्तार 50 किमी प्रति घण्टा से भी अधिक हो सकती है।

इन विनाशकारी समुद्री लहरों को ‘सूनामी’ कहा जाता है। ‘सूनामी’ जापानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों ‘सू’ अर्थात् ‘बन्दरगाह’ और ‘नामी’ अर्थात् ‘लहर’ से बना है। सूनामी लहरें अपनी भयावह शक्ति के द्वारा
विशाल चट्टानों, नौकाओं तथा अन्य प्रकार के मलबे को भूमि पर कई मीटर अन्दर तक धकेल देती हैं। ये तटवर्ती इमारतों, वृक्षों आदि को नष्ट कर देती हैं। 26 दिसम्बर, 2004 ई० को दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों में ‘सूनामी’ द्वारा फैलायी गयी विनाशलीला से सभी परिचित हैं। इन सूनामी लहरों की ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराये गये बम से तीन सौ पचास गुना अधिक पायी गयी थी।
कारण
सूनामी लहरों की उत्पत्ति के प्रधान कारण निम्नलिखित हैं—
1. ज्वालामुखी विस्फोट– महासागरों की तली के आन्तरिक भागों में जब कभी कोई ज्वालामुखी सक्रिय होता है और उसमें विस्फोट हो जाता है तो महासागरों में सूनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। सन् 1983 ई० में इण्डोनेशिया में क्रकटू नामक विख्यात ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ और इसके कारण लगभग 40 मीटर ऊँची सूनामी लहरें उत्पन्न हुईं। इन लहरों ने जावा व सुमात्रा में जन-धन को अपार क्षति पहुँचाई।
2. भूकम्प– समुद्र तल के पास या उसके नीचे भूकम्प आने पर समुद्र में हलचल पैदा होती है और यही हलचल विनाशकारी सूनामी का रूप धारण कर लेती है। 26 दिसम्बर, 2004 ई० को दक्षिण-पूर्व एशिया में आई विनाशकारी सूनामी लहरें भूकम्प का ही परिणाम थीं। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इन समुद्री लहरों को ‘भूगर्भिक बम’ कहते हैं। भारतीय भू-विज्ञानी प्रो० जे०जी० नेगी के अनुसार 26 दिसम्बर, 2004 ई० को आई भूकम्पजनित (UPBoardSolutions.com) प्रलयंकारी समुद्री लहरों की ताकत 32,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर थी।
3. भूस्खलन– समुद्र की तलहटी में भूकम्प व भूस्खलन के कारण ऊर्जा निर्गत होने से भी बड़ी-बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं जिनकी गति अत्यन्त तेज होती है। मिनटों में ही ये लहरें विकराल रूप धारण कर तट की ओर दौड़ती हैं। हाल ही के वर्षों में किसी बड़े क्षुद्र ग्रह (उल्कापात) के समुद्र में गिरने को भी समुद्री लहरों का कारण माना गया है।

प्रश्न 7. आपदा से आप क्या समझते हैं ? मानवकृत किन्हीं दो आपदाओं का वर्णन कीजिए। [2011, 12, 13, 17]
या
मानवीय आपदा का क्या तात्पर्य है? किसी एक मानवीय आपदा से बचने के लिए चार सुझाव दीजिए। [2015]
या
मानवकृत आपदा का क्या अभिप्राय है? ग्रीसहाउस के दो प्रभाव लिखिए। [2015]
उत्तर :
आपदा उसे प्राकृतिक या मानव-जनित भयानक घटना या संकट को कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य को शारीरिक चोट व मृत्यु तथा धन-सम्पदा, जीविका व पर्यावरण की हानि का दु:खद सामना करना पड़ता है। मानवकृत आपदाएँ मनुष्य की गलतियों एवं दुष्कर्मों का प्रतिफल होती हैं। मानवकृत दो आपदाओं का वर्णन इस प्रकार है
(1) ओजोन क्षरण
[ संकेत-इसके वर्णन के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखें।]
(2) हरितगृह प्रभाव
हरितगृह से तात्पर्य एक ऐसे गृह से है जो काँच का बना होता है। यह ताप को अन्दर तो आने देता है किन्तु बाहर नहीं जाने देता है। पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है किन्तु वायुमण्डल अपनी अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त करता है (पार्थिव विकिरण)। वायुमण्डले प्रवेशी लघु तरंग सौर्य विकिरण से प्रायः पारदर्शक होता है। वास्तव में वायुमण्डल काँच के घर की तरह होता है सूर्य के प्रकाश को बाहर से अन्दर आने तो देता है परन्तु (UPBoardSolutions.com) उस प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है। इसी प्रकार वायुमण्डल सौर्य विकिरण तरंगों को भूतल तक तो आने देता है किन्तु धरातल से होने वाली दीर्घ तरंगीय बहिर्गामी पार्थिव विकरण को बाहर जाने से रोकता है। वायुमण्डल के इस प्रभाव को ही हरितगृह प्रभाव कहते हैं।

हरितगृह प्रभाव के कारण
हरितगृह प्रभाव को कार्बन डाई-ऑक्साइड गैस के साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, जलवाष्प एवं आजोन, आदि गैसें भी बढ़ा रही हैं। पिछले 100 वर्षों में वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 25% वृद्धि हुई है। वायुमण्डल में इन हरित गृह गैसों की वृद्धि के अग्रलिखित कारण हैं—
- जीवाश्म ईंधन; जैसे-लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के जलने से।
- स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से।
- कल-कारखानों व औद्योगिक भट्ठियों में ईंधन के जलने से।
- ज्वालामुखी के उद्गार से।
- वनस्पति के सड़ने गलने से।
- वन-विनाश से।
हरितगृह प्रभाव के दुष्प्रभाव
पिछले 100 वर्षों में भूमण्डलीय औसत तापमान में 0.3°C से 0.7°C की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार सन् 2050 तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5°C से 4.5°C बढ़ने की सम्भावना है। ऐसा होने पर वर्तमान पर्यावरणीय व्यवस्था में वर्षा के प्रारूप (UPBoardSolutions.com) में परिवर्तन हो सकता है, बढ़ती गर्मी के कारण एलनिनो प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, हिमनदों की बर्फ पिघल सकती है और ध्रुवों पर जमी बर्फ की चादरों के पिघलने से, समुद्र तल एक मीटर ऊँचा हो सकता है तथा तटीय प्रदेश पानी में डूब सकते हैं।

हरित गृह के दुष्प्रभावों के नियन्त्रण के उपाय
हरित गृह प्रभाव को नियन्त्रण में करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं
1. वृक्षारोपण करना- वृक्षारोपण से वायुमण्डल में उपस्थित CO, की मात्रा, जो हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस है, कम हो जायेगी।
2. फैक्ट्रियों पर नियन्त्रण- फैक्ट्रियों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायुमण्डल को दूषित तो करती ही हैं, साथ ही हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती हैं। रसायन उद्योगों से निकलने वाली CO,, SO, (कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड) अत्यन्त हानिकारक
3. नाइट्रस ऑक्साइड (NO,)- जेट विमानों से निकलने वाली विषैली गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव को … बढ़ावा देती हैं।
4. CFC गैसों पर रोक-क्लोरो- फ्लोरो कार्बन, मीथेन (CH,) तथा (CO) कार्बन मोनोऑक्साइड ‘, वायुमण्डल को प्रदूषित कर हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती हैं तथा इन पर नियन्त्रण आवश्यक है।

प्रश्न 8.
भूमण्डलीय तापेन से आप क्या समझते हैं? इसके दो कारण एवं दो प्रभाव लिखिए। [2014]
उत्तर :
भूमण्डलीय तापन
गत 100 वर्षों में भूमण्डलीय औसत तापमान में लगभग 0.3°C से 0.7°C की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार सन् 2050 तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5°C से 4.5°C की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
भूमण्डलीय औसत तापमान में यह बढ़ोत्तरी ही. भू-मण्डलीय तापन कहलाती है।
कारण
भू-मण्डलीय तापन के दो प्रमुख कारण निम्नवत् हैं
- जीवाश्मी ईंधनों के बिना सोचे-समझे अधिक उपयोग से।।
- ओजोन छिद्र के कारण भूमण्डल पर पहुँचने वाली पराबैंगनी किरणों से।

प्रभाव
भू-मण्डलीय तापन के दो प्रमुख प्रभाव निम्नवत् हैं
- भूमण्डलीय तापन के कारण भूमण्डल की जलवायु में परिवर्तन हो जायेगा अर्थात् कहीं अधिक ठंड तो . कहीं अधिक गर्मी पड़ेगी, कहीं अधिक वर्षा होगी तो कहीं वर्षा नहीं होगी। जिसके कारण जन-जीवन प्रभावित होगा।
- भू-मण्डलीय तापन के कारण ग्लेशियर हिमनद, ध्रुवों तथा पर्वत की चोटियों (UPBoardSolutions.com) पर जमी बर्फ पिघल जायेगी जिसके कारण समुद्र तल की ऊँचाई बढ़ जायेगी फलस्वरूप समुद्र तटीय प्रदेश समुद्र में डूब जायेंगे।
लघु उत्तरीय प्रत
प्रश्न 1.
भुकम्प की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है ?
उत्तर :
भूकम्प की भविष्यवाणी निम्नलिखित तरीकों के द्वारा की जा सकती है
- किसी क्षेत्र में हो रही भूगर्भीय गतियों का उस क्षेत्र में हो रहे भू-आकृतिक परिवर्तनों से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि ऊपर-नीचे होती रहती है, अत्यधिक भूस्खलन होते हैं, नदियों के मार्ग में असामान्य परिवर्तन होता है, प्रायः भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं।
- किसी क्षेत्र में सक्रिय भ्रंशों, जिन दरारों से भूखण्ड टूटकर विस्थापित भी हुए हों, की उपस्थिति को भूकम्पे का संकेत माना जा सकता है। इस प्रकार के भ्रंशों की गतियों को समय के अनुसार तथा अन्य उपकरणों से मापा जा सकता है।
- भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में भूकम्पमापी यन्त्र (Seismograph) लगाकर विभिन्न भूगर्भीय गतियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इस अध्ययन से बड़े भूकम्प आने की पूर्व चेतावनी मिल जाती है। भूकम्प की आरम्भिक अवस्था में दरवाजे, खिड़कियाँ (UPBoardSolutions.com) व अन्य खिसकने और घूमने वाली वस्तुओं में कम्पन होने लगता है, या वे घूमने लगती हैं। मन्दिरों की घण्टियाँ भी बजने लगती हैं। यद्यपि भूकम्प का पूर्वानुमान अभी भी पूर्णतया सम्भव नहीं है, तथापि भूकम्प आने के पूर्व की ऐसी ही घटनाओं और व्यवहारों के अवलोकन और पहचान में दक्षता प्राप्त कर ली जाए तो भूकम्प आने से पूर्व आवश्यक सावधानियों द्वारा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।

प्रग 2.
भूकम्प आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
भूकम्प आपदा के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए
- भूकम्प के दौरान बौखलाहट तथा डर को मन में उत्पन्न न होने दें।
- जहाँ हैं वहीं टिके रहें परन्तु दीवारों, छतों और दरवाजों से दूर रहें। यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र मैदान, आँगन आदि खुले भाग में चले जाएँ। यदि खुले भाग में न जा सकें तो मेज या पलँग के नीचे चले जाएँ।
- दरारों के टूटने या मलबा गिरने पर गहरी नजर रखें। दीवारों या भारी सामान से दूर रहें तथा आँखों को हाथों से ढककर सुरक्षित कर लें।
- यदि चलती कार में हों तो गाड़ी रोककर बाहर आ जाएँ। भूकम्प के दौरान वाहन न चलाएँ तथा पुल या सुरंग भूलकर भी पार न करें।
- बिजली के मुख्य स्विच व गैस का पाइप बन्द कर दें और गैस-सिलिण्डर सील कर दें।
प्रश्न 3.
सूखा आपदा निवारण के प्रमुख उपाय लिखिए। [2012]
उत्तर :
सूखा आपदा निवारण के उपाय निम्नलिखित हैं
1. हरित पट्टियाँ- सड़क मार्गों के दोनों ओर 5 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टियों का विकास किया जाना चाहिए। हरित पट्टी कालान्तर में वर्षा की मात्रा में वृद्धि तो करती ही है, साथ ही यह वर्षा के जल को रिसकर भूतल के नीचे जाने में सहायक भी होती है। (UPBoardSolutions.com) इसके परिणामस्वरूप कुओं, तालाबों आदि में जल-स्तर बढ़ जाता है और मानव-उपयोग के लिए अधिक जल उपलब्ध हो जाता है।
2. जल-संचय- वर्षा कम होने की स्थिति में जल आपूर्ति को बनाये रखने के लिए, जल को संचय करके रखना एक दूरदर्शी युक्ति है। जल का संचय बाँध बनाकर या तालाब बनाकर किया जा सकता। है। प्राकृतिक तालाबों का संरक्षण भी एक उत्तम उपाय है। इनमें जल का संचय भू-जल के स्तर को भी ” बढ़ाता है।
3. वर्षा-जल का संचय- वर्षा-जले का अधिकाधिक संचय किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं नगरीय | क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्वामी के द्वारा वर्षा-जल का संचय अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह जलसिंचन, पशुओं, मल-निकास आदि से सम्बद्ध कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। राजस्थान के एक गाँव ने इसी पद्धति को अपनाकर अपने तथा आसपास के गाँवों की जल-समस्या को दूर कर दिया है।
4. नदियों को आपस में जोड़ने से देश की विभिन्न सततवाहिनी नदियों को आपस में जोड़ने से उन क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध किया जा सकता है, जहाँ वर्षा का अभाव रहा हो। भारत सरकार नदियों को जोड़ने की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना अगस्त, 2005 ई० में प्रारम्भ कर चुकी है।

5. भूमि का उपयोग- सूखा सम्भावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, विशेषकर हरित पट्टी बनाने के लिए कम-से-कम 35% भूमि को आरक्षित कर दिया जाना चाहिए और इस भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना (UPBoardSolutions.com) चाहिए। हरित पट्टी बनाने के लिए वृक्षों एवं फसलों का चयन विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करना चाहिए।
प्रश्न 4.
नाभिकीय परमाणु विस्फोट के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके निवारण के कोई दो प्रमुख उपाय लिखिए।
उत्तर :
नाभिकीय विस्फोटों के पीछे निम्नलिखित दो मूल कारण निहित हैं
- मानवीय भूल, तकनीकी अकुशलता या कुंप्रबन्ध एवं अव्यवस्था, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु ईंधन , संयन्त्रों में विस्फोट या रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव के कारण तबाही की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- मानवीय दुष्प्रवृत्तियाँ जो राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत उत्पन्न होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा
राजनीतिक स्वार्थों के कारण ही दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था।
नाभिकीय विस्फोट एवं रिसाव से बचने की सबसे प्रभावशाली युक्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बमों के निर्माण व प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध एवं परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में पूर्ण सावधानी रखने से हो सकती है। इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके निर्माण तथा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की तत्काल आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय; विशेष रूप से अमेरिका; को मानव कल्याण के लिए पूर्ण इच्छाशक्ति व ईमानदारी से ऐसे प्रतिबन्धों का पालन करना चाहिए। ऊर्जा संयन्त्रों से उत्पन्न विकिरण के खतरों को न्यूनतम करने हेतु निम्नलिखित दो उपाय हैं
- परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से उत्पन्न कचरे के निस्तारण का ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे रेडियोधर्मी विकिरण न हो। रेडियोसक्रिय अवशिष्टों तथा उच्चस्तरीय द्रव्य अवस्था के कचरों को गन्धक व पिच के साथ मिश्रित करके ठोस बनाकर स्टील के ड्रमों में सुरक्षित कर उन्हें समुद्र की अगाध गहराई में ड्रिल किये गये गत में दबाया जा सकता है।
- रिऐक्टरों के रख-रखाव में पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। (UPBoardSolutions.com) समय-समय पर परमाणु संयन्त्रों व पाइप लाइनों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहाँ से गैसों का रिसाव हो सकता है, वहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 5.
चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात से आप क्या समझते हैं? [2011]
या
चक्रवात से आप क्या समझते हैं ? [2010]
उत्तर :
चक्रवात( समुद्री तूफान)- चक्रवात एक प्रकार की पवनें हैं जो उष्ण कटिबन्ध में तीव्र गति से चलती हैं। यह एक निम्न दाब का क्रम होता है जिसमें बाहर की ओर से केन्द्र की ओर हवाएँ तीव्र गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में ये हवाएँ घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलती हैं किन्तु दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की अनुकूल दिशा में ये पवनें चला करती हैं। यह चक्रवात मौसमी होते हैं। ये प्राय: ग्रीष्मकाल के उत्तरार्द्ध में सक्रिय होते हैं। इनकी उत्पत्ति तापीय भिन्नता के कारण होती है। वास्तव में यह तेज गति से लचने वाली विनाशकारी पवनें होती हैं। इनके चलने की दिशा प्राय: पश्चिम की ओर होती है तथा इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घण्टा से भी अधिक होती है। समुद्र में तो यह तीव्र गति से चलती हैं किन्तु तटों पर पहुँचने पर स्थल से घर्षण होने के फलस्वरूप कमजोर पड़ जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में इन्हें ‘चक्रवात’, ऑस्ट्रेलिया में ‘विली विलीज’, संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘हरीकेन’ तथा चीन में ‘टाइफून’ कहा जाता है।
प्रतिचक्रवात- चक्रवातों के विपरीत प्रतिचक्रवात, उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इन उच्च वायुदाब केन्द्रों से वायु का प्रवाह बाहर की ओर होता है। वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सूइयों के विपरीत दिशा में होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की उच्च वायुदाब पेटियाँ और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र इनकी उत्पत्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं। चक्रवातों की अपेक्षा प्रतिचक्रवातों का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर कम बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रतिचक्रवात वायु के नीचे उतरने के क्षेत्र होते हैं। नीचे उतरती वायु धरातल पर उच्च वायुदाब बनाए रखती है तथा बाहर की ओर फैलती है। सामान्यतया प्रतिचक्रवात स्वच्छ मौसम लाते हैं परंतु यह सदैव सच नहीं होता है। कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में प्रतिचक्रवातों में कपासी तथा कपासी वर्षा मेघों की (UPBoardSolutions.com) उत्पत्ति होने से यह धारणा गलत सिद्ध होती है। प्रतिचक्रवात के केन्द्र की ओर वायुदाब प्रवणता कमजोर होती है और पवनें हल्की तथा परिवर्तनशील होती हैं।
प्रश्न 6.
भूकम्प से बचाव के उपाय लिखिए।
उत्तर :
भूकम्प से बचाव के उपाय-भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोक पाना मनुष्य के वश में नहीं है। भूकम्प से होने वाली हानि को निम्नलिखित उपायों द्वारा से कम अवश्य किया जा सकता है–
- किसी क्षेत्र में हो रही भूगर्भीय गतियों का उस क्षेत्र में हो रहे भू-आकृतिक परिवर्तनों से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमि ऊपर-नीचे होती रहती है, अत्यधिक भूस्खलन होते हैं, नदियों के मार्ग में असामान्य परिवर्तन होता है, प्रायः भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं।
- किसी क्षेत्र में सक्रिय भ्रंशों, जिन दरारों से भू-खण्ड टूटकर विस्थापित भी हुए हों, की उपस्थिति को भूकम्प का संकेत माना जा सकता है। इस प्रकार के भ्रंशों की गतियों को समय के अनुसार तथा अन्य उपकरणों से नापा जा सकता है।
- भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में भूकम्पमापी यन्त्र (Seismograph) लगाकर विभिन्न भूगर्भीय गतियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इस अध्ययन से बड़े भूकम्प आने की पूर्व चेतावनी मिल जाती है।
- यद्यपि भूकम्प का पूर्वानुमान अभी भी पूर्णतया सम्भव नहीं है, तथापि बड़े भूकम्प आने से पहले कुछ असामान्य प्राकृतिक घटनाएँ तथा जैविक व्यवहार घटित होने लगते हैं। यदि इन घटनाओं और व्यवहारों के अवलोकन और पहचान में दक्षता प्राप्त कर ली जाए तो भूकम्प आने से पूर्व आवश्यक सावधानियों द्वारा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
- मनुष्य से अधिक संवेदनशील प्राणी; जैसे—कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, चमगादड़ आदि तथा कुछ अन्य जानवर अचानक उत्तेजित होकर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, जिसे पहचाना जा सकता है। इस असामान्य व्यवहार का कारण सम्भवतः भूकम्प आने से पूर्व पृथ्वी की कमजोर सतहों से निकलने वाली । ऊर्जा एवं विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इनको आधुनिक उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है।
- जलीय स्रोतों का पानी गन्दा अथवा मटमैला होने लगता है। रुके हुए पानी के गड्ढों की सतह में उपस्थित कीचड़ में सूक्ष्म मोड़ पड़ने लगते हैं।
- भूकम्प आने से पूर्व पृथ्वी की रेडियोधर्मिता में हुई असामान्य वृद्धि से गैसों के निकलने के कारण वातावरण में अचानक परिवर्तन; जैसे-हेवा का शान्त हो जाना, तेज आँधी या तूफान आना आदि; अनुभव किये जाते हैं।
- भूकम्प की आरम्भिक अवस्था में दरवाजे, खिड़कियाँ व अन्य खिसकने और घूमने वाली वस्तुओं में कम्पन होने लगता है या वे घूमने लगती हैं। मन्दिरों की घण्टियाँ भी बजने लगती हैं। अत: उपर्युक्त लक्षणों की पहचान हो जाने पर भूकम्प से बचने की तैयारी प्रारम्भ कर लेनी चाहिए, जिससे होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

प्रश्न 7.
भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखिए तथा सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर :
भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र को निम्नलिखित प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है-
1. मरुस्थलीय क्षेत्र– भारत में राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्र अत्यधिक सूखे के प्रकोप का सामना करता है। यहाँ प्रत्येक दो या तीन वर्षों के अन्तराल पर भीषण सूखा पड़ता रहता है।
2. गुजरात, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश- इन क्षेत्रों में प्रायः तीन वर्ष बाद (UPBoardSolutions.com) सूखा पड़ता रहता है। पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण अब अधिकतर सूखे की समस्या बनी रहती है।
3. तमिलनाडु, रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्र- इन क्षेत्रों में दो से ढाई वर्ष के अन्तराल पर सूखा संकट का सामना करना पड़ता है। अत: इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत रखा जाता है।
4. पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी मैसूर एवं विदर्भ क्षेत्र- इन क्षेत्रों में सामान्यत: चार या इससे अधिक वर्षों | में सूखे का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों को मध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है।
5. पश्चिम बंगाल, पूर्वी तटीय प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश- इन क्षेत्रों में औसतन पाँच वर्ष या इससे अधिक समय में सूखा संकट का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों के विस्तार में कभी-कभी बिहार एवं झारखण्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं। ये क्षेत्र निम्न सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत माने जाते हैं।
सूखा पड़ने के प्रमुख कारण
[ संकेत-इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखें। ]

प्रश्न 8.
बाढ़ प्रकोप के कारणों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर :
बाढ़ प्राकृतिक एवं मानवजनित दोनों कारकों को परिणाम है। प्राकृतिक कारकों में लम्बी अवधि तक उच्च तीव्रता वाली जल-वर्षा, नदियों के घुमावदार मोड़ व स्वाभाविक अवरोध, भूस्खलन आदि प्रमुख हैं, तो मानवजनित कारकों में नगरीकरण, नदियों पर बाँधों का निर्माण, पुलों व जलभण्डारों का निर्माण, अत्यधिक वन-विनाश आदि प्रमुख हैं। भारत में बाढ़ आपदा के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं
1. निरन्तर भारी वर्षा- जब किसी क्षेत्र में निरन्तर भारी वर्षा होती है तो वर्षा का जल धाराओं के रूप में मुख्य नदी में मिल जाता है। यह जल नदी के तटबन्धों को तोड़कर आस-पास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। भारी मानसूनी वर्षा तथा चक्रवातीय वर्षा बाढ़ों के प्रमुख कारण हैं।
2. भूस्खलन- भूस्खलन भी कभी-कभी बाढ़ों का कारण बनते हैं; क्योंकि इसके कारण नदी का मार्ग ‘अवरुद्ध हो जाता है। परिणामस्वरूप नदी का जल-मार्ग बदलकर आस-पास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। इस प्रकार की बाढ़ का वेग इतना तीव्र होता (UPBoardSolutions.com) है कि यह बड़ी-से-बड़ी बस्ती को भी अस्तित्वविहीन कर देता है।
3. वन-विनाश- वन पानी के वेग को कम करते हैं। नदी के ऊपरी भागों में बड़ी संख्या में वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई से भी बाढ़े आती हैं। हिमालय में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश ही हिमालय-नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण है। वनविहीन भूमि पर वर्षा का जल तेजी से बहता है, जिससे भूमि का कटाव अधिक होता है। इससे नदियों में अधिक मात्रा में अवसाद एकत्रित होता है और नदियों का तल उथला होता जा रहा है।
4. दोषपूर्ण जल- निकास प्रणाली- मैदानी क्षेत्रों में उद्योगों और बहुमंजिले मकानों की परियोजनाएँ बाढ़ की सम्भावनाओं को बढ़ाती हैं। इसका कारण यह है कि पक्की सड़कें, नालियाँ, निर्मित क्षेत्र, पक्के पार्किंग स्थल आदि के कारण यहाँ जल रिसकर भू-सतह के नीचे नहीं जा पाता और जल निकास की भी पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्षा का पानी निचले स्थानों पर भरता चला जाता है। तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
5. बर्फ का पिघलना- सामान्य से अधिक बर्फ का पिघलना भी बाढ़ का एक कारण है। बर्फ के अत्यधिक पिघलने से नदियों में जल की मात्रा उसी अनुपात में अधिक हो जाती है तथा नदियों का जल तटबन्धन तोड़कर आस-पास के इलाकों को जलमग्न कर देता है। (UPBoardSolutions.com) उपर्युक्त के अतिरिक्त कभी-कभी अचानक बाँध, तटबन्ध या बैराज के टूटने से भी प्रचण्ड बाढ़ आ जाती है। वर्तमान में अतिशय जनसंख्या-वृद्धि के कारण भूमि का उपयोग बड़ी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जल-निकासी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जल-भराव या बाढ़ की विकट समस्या उत्पन्न होती जा रही है।

प्रश्न 9.
सूनामी लहरों से बचाव के उपाय लिखिए।
उत्तर :
यदि आप किसी ऐसे तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं कि जहाँ सूनामी की आशंका है, तो आपको बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए
- समुद्रतट के समीप न तो मकान बनवाएँ और न ही किसी तटवर्ती बस्ती में रहें। यदि तट के समीप रहना आवश्यक हो, तो घर को यथासम्भव अत्यधिक ऊँचे स्थान पर बनवाएँ। अपने घरों को बनवाते समय भवन-निर्माण विशेषज्ञ की राय लें तथा मकान को सूनामी निरोधक बनवाएँ।
- तटीय ज्वार जाली का निर्माण करके, सूनामियों को तट के निकट रोका जा सकता है। गहरे समुद्र में | इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- सूनामी के विषय में प्राप्त चेतावनी के प्रति लापरवाही न बरतें तथा यदि समुद्री लहरों से प्रभावित क्षेत्र में रहते हों तो समुद्रतट से दूर किसी सुरक्षित ऊँचे स्थान पर चले जाएँ।
- सूनामी की चेतावनी सुनते समय यदि आप समुद्र में किसी जलयान पर हों तो किनारे पर लौटने के स्थान पर जलयान को गहरे समुद्र की ओर ले जाएँ; क्योंकि सूनामी का सर्वाधिक कहर किनारों पर ही होता है।
- ऊँची इमारतें यदि मजबूत कंक्रीट की बनी हों तो खतरे के समय इसकी ऊपरी मंजिल को सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- पानी के साथ मकान में घुस आये जहरीले जीव-जन्तुओं, सर्प आदि से सतर्क रहें। मलबा हटाने के लिए भी उपयुक्त उपकरण का प्रयोग करें।
प्रश्न 10.
रासायनिक एवं विस्फोटजनित आपदाओं के कारणों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर :
रासायनिक व औद्योगिक विस्फोटजनित आपदाओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
- उद्योगों का अनियोजित विकास।
- उचित प्रबन्धन एवं सुरक्षा उपायों के साथ मानवीय त्रुटियों व तकनीकी कुशलता का अभाव।
- प्रबन्धकों द्वारा निर्धारक मानकों की अवहेलना।
- औद्योगिक क्षेत्रों का मानव बस्तियों के निकट स्थापित होना।
- जोखिमयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान से जनसामान्य का अनभिज्ञ रहना।
उपर्युक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त कभी-कभी इस प्रकार की दुर्घटनाएँ (UPBoardSolutions.com) कुछ प्राकृतिक कारणों; जैसे—बाढ़, भूकम्प या आग लगने के कारण भी घटित हो जाती हैं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
प्राकृतिक आपदा क्या है? किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए। [2013, 14]
उत्तर :
प्राकृतिक कारणों से या प्रकृति के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। दो प्राकृतिक आपदाएँ हैं-भूकम्प तथा सूनामी।
प्रश्न 2.
भूकम्प की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं ?
उत्तर :
भूकम्प की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं
- ज्वालामुखी उद्गार,
- भू-असन्तुलन में अव्यवस्था,
- जलीय भार,
- भू-पटल में सिकुड़न,
- प्लेट विवर्तनिकी,
- संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
प्रश्न 3.
ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर :
भूकम्प के समान ज्वालामुखी प्रक्रिया भी इतनी शीघ्र एवं आकस्मिक रूप से घटती है कि भू-पृष्ठ पर इसका विनाशकारी प्रभाव दिखायी देता है। इसमें भूगर्भ से अत्यन्त ऊँचे तापमान पर लावा, गैस, राख इत्यादि पदार्थ तीव्र गति से विस्फोट के साथ (UPBoardSolutions.com) निकलते हैं। इससे काफी धन-जन की हानि होती है।
प्रश्न 4.
भूस्खलन किसे कहते हैं ?
उत्तर :
भूमि के एक सम्पूर्ण भाग अथवा उससे विखण्डित एवं विच्छेदित खण्डों के रूप में खिसक जाने अथवा गिर जाने को भूस्खलन कहते हैं।

प्रश्न 5.
बाढ़ प्रकोप के प्रमुख कारण क्या हैं ?
उत्तर :
बाढ़ प्रकोप के प्रमुख कारण हैं-
- निरन्तर भारी वर्षा,
- भूस्खलन,
- वन-विनाश,
- दोषपूर्ण जल-निकास प्रणाली,
- बर्फ का पिघलना।
प्रश्न 6.
सूनामी किसे कहते हैं ?
या
सूनामी शब्द की व्याख्या कीजिए।
उत्तर :
‘सूनामी’ जापानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों-‘सू’ अर्थात् बन्दरगाह तथा ‘नामी’ अर्थात् लहर से बना है। सूनामी को ‘समुद्री लहरें भी कहा जाता है।
प्रश्न 7.
आपदा से क्या तात्पर्य है? [2012, 18]
उत्तर :
आपदा उसे प्राकृतिक या मानव-जनित भयानक घटना या संकट को कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य को शारीरिक चोट व मृत्यु का तथा धन-सम्पदा, जीविका व पर्यावरण की हानि का दु:खद सामना करना पड़ता है।

प्रश्न 8.
भूकम्प केन्द्र से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर :
जिस स्थान पर भूकम्पीय लहरों को अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है, उसे भूकम्प केन्द्र या अभिकेन्द्र कहते हैं तथा भूगर्भ में चलने वाली भूकम्पीय लहरों का प्रारम्भ जिस स्थान से होता है, उसे भूकम्प मूल कहते हैं।
प्रश्न 9.
भूस्खलन का एक मानवजनित कारण लिखिए।
उत्तर :
वनों की अन्धाधुन्ध कटाई और पहाड़ों पर बड़े बाँध व बड़ी इमारतें बनाने से पहाड़ों पर बढ़ता दबाव भूस्खलन का एक मानवजनित कारण है।
प्रश्न 10.
हरित पट्टी की एक उपयोगिता लिखिए।
उत्तर :
हरित पट्टी कालान्तर में वर्षा की मात्रा बढ़ाती है तथा यह वर्षा जल को रिसकर भूतल के नीचे जाने में सहायक भी होती है।
प्रश्न 11.
अधिक बर्फ पिघलने से बाढ़ कैसे आती है ?
उत्तर :
सामान्य से अधिक बर्फ का पिघलना भी बाढ़ का एक कारण है। बर्फ के (UPBoardSolutions.com) अत्यधिक पिघलने से, नदियों में जल की मात्रा उसी अनुपात में अधिक हो जाती है तथा नदियों का जल तट-बन्धन तोड़कर आस-पास के इलाकों को जलमग्न कर देता है।

प्रश्न 12.
आपदा प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं? [2015]
उत्तर :
प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने को आपदा प्रबन्धन कहते हैं।
बहुविकल्पीय
प्रश्न 1. प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं
(क) जन्तुजनित ।
(ख) मानवजनित
(ग) वनस्पतिजनित
(घ) प्रकृतिजनित
2. निम्नलिखित में कौन-सी प्राकृतिक आपदा नहीं है?
(क) ज्वालामुखी विस्फोट
(ख) जनसंख्या विस्फोट
(ग) बादल विस्फोट
(घ) चक्रवात
3. भू-प्लेटों के खिसकने से क्या होता है?
(क) ज्वालामुखी विस्फोट
(ख) चक्रवात
(ग) बाढ़
(घ) सूखा
4. विश्व में सर्वाधिक भूकम्प कहाँ आते हैं?
(क) जापान
(ख) भारत
(ग) इटली
(घ) सिंगापुर

5. भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कौन-सा क्षेत्र है?
(क) पहाड़ी प्रदेश
(ख) मैदानी भाग
(ग) पठारी प्रदेश
(घ) ये सभी
6. अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं?
(क) बाढ़
(ख) सूखा
(ग) भूस्ख लन
(घ) सूनामी
7. अनावृष्टि से होने वाली आपदा को क्या कहते हैं?
(क) चक्रवात
(ख) सूखा
(ग) सूनामी
(घ) आग
8. निम्न गैसों में से किस गैस को ‘ग्रीनहाउस गैस’ के नाम से जानते हैं?
(क) ओजोन
(ख) कार्बन डाइऑक्साइड
(ग) क्लोरीन
(घ) ऑक्सीजन

9. सागरों में भूकम्प के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं?
(क) सूनामी
(ख) चक्रवात
(ग) भूस्खलन
(घ) ज्वार-भाटा
10. निम्नलिखित में से कौन-सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? [2012, 14, 17]
(क) सूखा
(ख) चक्रवात
(ग) रेल दुर्घटना
(घ) सूनामी
11. निम्नलिखित में से कौन आपदा मानव-निर्मित है? [2013]
(क) भूस्खलन
(ख) भूकम्प
(ग) हरितगृह प्रभाव प्रभाव
(घ) सूनामी लहरें
12. सूनामी है [2014]
(क) एक नदी
(ख) एक पवन
(ग) एक पर्वत चोटी
(घ) एक प्राकृतिक आपदा
13. वैश्विक तपन का प्रभाव है [2014]
(क) बाढ़
(ख) सूखा
(ग) चक्रवात
(घ) ये सभी

14. निम्नलिखित में से कौन-सी एक मानवकृत आपदा है? [2016]
(क) भूस्खलन
(ख) भूकम्प
(ग) बाढ़
(घ) बम विस्फोट
15. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? [2017]
(क) पर्वतीय क्षेत्र
(ख) पठारी क्षेत्र
(ग) मैदानी क्षेत्र
(घ) समुद्रतटीय क्षेत्र

16. निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? [2017]
(क) सूनामी
(ख) बाढ़।
(ग) वैश्विक तापन
(घ) ज्वालामुखी विस्फोट
17. अनावृष्टि से होने वाली आपदा को कहा जाता है [2017]
(क) चक्रवात
(ख) सूनामी
(ग) बाढ़
(घ) सूखा उत्तरमाला
उत्तरमाला
1. (घ), 2. (ख), 3. (क), 4. (क), 5. (क), 6. (क), 7. (ख), 8. (ख), 9. (क), 10. (ग), 11. (ग), 12. (घ), 13. (घ) 14. (घ), 15. (क), 16. (ग) 17. (घ)।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 आपदाएँ (अनुभाग – तीन) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 आपदाएँ (अनुभाग – तीन), drop a comment below and we will get back to you at the earliest
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()