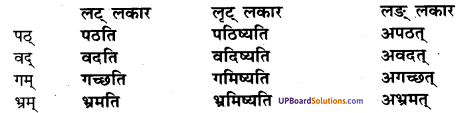UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 4 गृह-सज्जा (घर की सजावट)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Home Science Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Home Science गृह विज्ञान Chapter 4 गृह-सज्जा (घर की सजावट)
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की सजावट में आप किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगी? सजावट के महत्त्व का वर्णन कीजिए। [2007, 10, 17]
गृह-सज्जा केवल धन पर ही निर्भर नहीं करती, गृहिणी की कलात्मक रुचि पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। [2013]
गृह-सज्जा से क्या तात्पर्य है? गृह-सज्जा की क्या उपयोगिता है?
घर की सजावट (गृह-सज्जा) के बारे में लिखिए। घर की सजावट करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगी? [2008, 09, 10]
सुव्यवस्था एवं सजावट से क्या तात्पर्य है? सजावट के समय किन उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगी? [2016]
घर की सजावट करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखेंगी? [2016, 17, 18]
सजावट से क्या तात्पर्य है? [2016]
या
गृह-सज्जा क्या है? गृह-सज्जा क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। [2016]
उत्तर:
घर की सजावट से तात्पर्य
प्रत्येक वस्तु के सौन्दर्य एवं आकर्षण पक्ष का सम्बन्ध ‘कला’ से होता है। यह मनुष्य की विशिष्ट रुचि अथवा रुचियों की अभिव्यक्ति है। घर की सजावट का तात्पर्य इस बात से नहीं है कि घर में कीमती-से-कीमती वस्तुओं को इकट्ठा कर दिया जाए। (UPBoardSolutions.com) वास्तव में, घर की सजावट तो एक रचनात्मक कला है जो एक साधारण घर की भी कायाकल्प कर देती है। सजावटे ‘कला’ के नियमों पर ही आधारित होती है, क्योंकि सजावट में प्रयुक्त होने वाले साधनों में आकार, रंग एवं प्रकाश का ही महत्त्व होता है। अतः कला के मौलिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए घर में विभिन्न वस्तुओं की रुचिपूर्ण व्यवस्था को गृह-सज्जा अथवा घर की सजावट कहते हैं।
![]()
इस प्रकार स्पष्ट है कि घर की सजावट में कला तथा कल्पनाशीलता के समावेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। गृह-सज्जा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सुन्दरराज ने इन शब्दों में एक परिभाषा प्रस्तुत की है, “आन्तरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है…… यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है और इस प्रकार घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है।” प्रस्तुत परिभाषा द्वारा स्पष्ट है कि गृह-सज्जा द्वारा घर की दशा में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। इसके माध्यम से (UPBoardSolutions.com) घर का वातावरण अच्छा बन जाता है, घर आकर्षक प्रतीत होने लगता है। तथा घर को देखकर घर में रहने वालों की रुचि, कलात्मक दृष्टिकोण तथा सांस्कृतिक मूल्यों का अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है।
सजावट की उपयोगिता एवं महत्त्व
घर की सजावट की उपयोगिता एवं महत्त्व को वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं
(1) घर के आकर्षण में वृद्धि--सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित घर अतिथियों एवं घर के सदस्यों-दोनों ही के लिए प्रसन्नता एवं आकर्षण का केन्द्र होता है। यह भी कहा जा सकता है कि गृह-सज्जा से घर के आकर्षण में वृद्धि होती है।
(2) कलात्मक रुचि की अभिव्यक्ति सुसज्जित घर गृहिणी की कलात्मक रुचि का परिचायक होता है।
(3) सुख एवं सन्तोष की प्राप्ति-सुसज्जित घर की गृहिणी एवं परिवार के सभी सदस्य सदैव सुख एवं सन्तोष का अनुभव करते हैं।
(4) स्वास्थ्य लाभ में सहायक-स्वच्छ एवं सुसज्जित घर में कीटाणुओं के पनपने की सम्भावना अत्यन्त कम होती है तथा घर के सभी सदस्य प्रायः स्वस्थ रहते हैं।
(5) वस्तुओं की सुरक्षा–सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित घर में सभी वस्तुएँ उचित एवं 35 स्थान पर रखी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी टूट-फूट की सम्भावना लभग नगण्य रहती है।
(6) समय एवं श्रम की बचत-एक सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित घर में (UPBoardSolutions.com) वस्तुओं के : समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता हैं। आवश्यकता पड़ने पर इच्छित वस्तु तुरन्त मिल जाते है। इन ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि उचित गृह-सज्जा से समय एवं श्रम की बचत होतो है।
(7) सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि–घर की सजावट से गृहिण व घर के अन्य सदस्यों की कलात्मक रुचि, विवेक एवं कार्यक्षमता का पता चलता है। इस प्रकार एक सुत्ररित एवं सुसज्जित घर की गृहिणी एवं परिवारजन समाज में सदैव प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा के पा रहे हैं।
सजावट करते समय ध्यान देने योग्य बातें
घर की सजावट एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है, परन्तु सजावट करते समय अन एवं समय का विवेकपूर्ण उपयोग, अपनी आर्थिक क्षमता का ज्ञान, कला के भौलिक सिद्धान्तों का पालन इत्यादि अनेक कारकों को दृष्टिगत रखना भी अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा (UPBoardSolutions.com) अनेक असुविधाओं का सामना कर, सकता है। सामान्यत: घर की सजावट करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है
![]()
(1) आर्थिक क्षमता का ज्ञान-प्रत्येक गृहिणी को घर की सजावट करते समय पारिवारिक आय का ध्यान रखना चाहिए। उसे सजावट पर केवल उतना ही धन व्यय करना चाहिए जिससे कि परिवार की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा बचत पर कुप्रभाव न पड़े। उसे सजावट के लिए आय के अनुसार ही मूल्यवान सामग्री खरीदनी चाहिए।
(2) कला के मौलिक सिद्धान्तों का पालन–प्रत्येक गृहिणी को सजावट की वस्तुओं का प्रयोग करते समय उनके आकार, रंग, अनुरूपता, अनुपात इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
(3) सजावट की शैली का ध्यान–गृहिणी को अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के आधार पर सजावट की देशी अथवा विदेशी शैली को अपनाना चाहिए।
(4) सजावट की सामग्री का विवेकपूर्ण क्रय-सजावट की वस्तुएँ खरीदते समय उनकी मजबूती तथा उत्तमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
(5) सजावट की सामग्री का उचित चुनाव-प्राय: घर की आवश्यकता एवं (UPBoardSolutions.com) उपलब्ध स्थान के अनुसार ही सजावट की सामग्री खरीदनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सजावट की सामग्री; जैसे—सोफा, फर्नीचर, परदे इत्यादि के डिजाइन वे रंगों का रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चयन करना चाहिए।
(6) व्यवस्था का क्रम-सजावट की सामग्री को उचित स्थान पर रखना चाहिए; जैसे, सोफा, कलात्मक तस्वीरें इत्यादि बैठक अथवा ड्राइंग-रूम में रखी जानी चाहिए टी०वी० आदि का सयन कक्ष में रखा जा सकता है।
![]()
प्रश्न 2.
घर की सजावट के मूलभूत सिद्धान्त कौन-कौन से हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
घर की आन्तरिक सजावट के क्या सिद्धान्त हैं? इनकी क्या उपयोगिता है? [2012, 14]
या
घर की आन्तरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की सजावट के लिए किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? [2008, 11, 12]
या
भीतरी सजावट के प्रमुख सिद्धान्त लिखिए। [2007, 17, 18]
उत्तर:
घर की सजावट के सिद्धान्त जैसा कि हम जानते हैं कि गृह-सज्जा अपने (UPBoardSolutions.com) आप में एक व्यवस्थित कला एवं विज्ञान है; अतः गृह-सज्जा का कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होना स्वाभाविक है। विद्वानों ने गृह-सज्जा के तीन मुख्य
गृह-सज्जा (घर की सजावट) 55 सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। ये सिद्धान्त क्रमश:
इस प्रकार हैं–
- सुन्दरता,
- अभिव्यक्ति तथा
- उपयोगिता। गृह-सज्जा के इन तीनों सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय निम्नवर्णित है-
(1) सुन्दरता--गृह-सज्जा का मूलभूत तथा मुख्य सिद्धान्त है–सुन्दरता। आदिकाल से ही व्यक्ति सुन्दरता का उपासक है। व्यक्ति स्वभाव से ही सौन्दर्यप्रिय है तथा अपनी प्रत्येक वस्तु एवं पर्यावरण को सुन्दर एवं आकर्षक देखना चाहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है। कि गृह-सज्जा को उद्देश्य घर को सुन्दर एवं आकर्षक बनाना होता है। सुन्दरता के अभाव में किसी भी घर को सुसज्जित नहीं माना जा सकता, भले ही घर में असंख्य बहुमूल्य वस्तुएँ क्यों न एकत्र कर दी जाएँ।
सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकृत है कि सुसज्जित गृह को सुन्दर एवं आकर्षक होना चाहिए, (UPBoardSolutions.com) पत। प्रश्न यह उठता है कि सुन्दरता से क्या आशय है? सुन्दरता के अर्थ को प्रस्तुत करना इतना सरल नई है। यह एक जटिल प्रश्न है तथा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या की जाती रही है। भिन्न-भिन्न कालों में सुन्दरता के प्रतिमान बदलते रहे हैं।
![]()
इस कठिनाई के होते हुए भी सुन्दरता को परिभाषित करने के प्रयास सदैव होते रहे हैं। ए० एच० रट (A. H. Rutt) के शब्दों में, “सुन्दरता गुणों का वह संयोजन है, जो पारखी आँखों या कानों को सुखद लगे।” इसी से मिलती-जुलती परिभाषा सुन्दरराज ने इन शब्दों में प्रस्तुत की है, “सुन्दरता वह तत्त्व अथवा गुण है, जो इन्द्रियों को आनन्दित करता है तथा आत्मा को उच्च अनुभूति देता है।” इस कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सुन्दरता का सम्बन्ध हमारे शरीर तथा आत्मा दोनों से होता है। सुन्दरता सदैव आनन्ददायक होती है तथा उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। गृह-सज्जा में निहित सुन्दरता का अच्छा प्रभाव घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों पर पड़ता है।
घर की आन्तरिक सुन्दरता व्यक्ति एवं परिवार को सुख देने में सहायक होती है। अब प्रश्न उठता है कि गृह-सज्जा में सौन्दर्य का समावेश कैसे हो? इस विषय में रट महोदय का कहना है कि गृह-सज्जा में सौन्दर्य का विकास अध्ययन, निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा किया जा सकता है। आजकल प्राय: सभी पत्र-पत्रिकाओं में गृह-सज्जा सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार दूरदर्शन तथा फिल्मों के माध्यम से भी गृह-सज्जा में सौन्दर्य के तत्त्व को जाना जा सकता है। गृहिणी अपने अनुभवों द्वारा भी गृह-सज्जा को अधिक सुन्दर एवं आकर्षक बना सकती है। वर्तमान समय में दूरदर्शन के प्रायः सभी धारावाहिक अपने मूल (UPBoardSolutions.com) कथानक के प्रदर्शन के साथ-ही-साथ गृह-सज्जा एवं उत्तम जीवन-शैली को भी दर्शाया करते हैं।
(2) अभिव्यक्ति-गृह-सज्जा का एक सिद्धान्त अभिव्यक्ति या अभिव्यंजकता भी है। गृह-सज्जा के माध्यम से कुछ-न-कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। इसी अभिव्यक्ति के आधार पर गृह-सज्जा का मूल्यांकन किया जाता है। अभिव्यक्ति एक व्यक्तिगत विशेषता मानी जा सकती है, जो गृह-सज्जा द्वारा प्रकट होती है। इस तथ्य को सुन्दरराज ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है, “यह वह गुण है, जो एक घर को दूसरे से भिन्न बनाता है। यह घर में रहने वाले सदस्यों के व्यक्तित्व को स्पष्टतः प्रतिबिम्बित करता है।”
अब प्रश्न उठता है कि गृह-सज्जा के सन्दर्भ में अभिव्यक्ति का क्या स्थान एवं महत्त्व है? इस विषय में टी० एफ० हेमलिन (T. F. Hamlin) ने स्पष्ट किया है, “प्रत्येक भवन, प्रत्येक सुनियोजित कक्ष में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह हमें आनन्द, शान्ति अथवा शक्ति का सन्देश दे सके।” स्पष्ट है कि गृह-सज्जा से भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। गृह-सज्जा के माध्यम से विश्रांति, जीवन्तता, स्वाभाविकता, आत्मीयता, औपचारिकता तथा दृढ़ता आदि भावनाएँ प्रकट होती हैं।
इस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली गृह-सज्जा को उत्तम गृह-सज्जा माना जाता है। इससे भिन्न यदि किसी गृह-सज्जा से भड़कीलापन या सुरुचि एवं स्वच्छता की कमी अभिव्यक्त होती हो तो उस गृह-सज्जा को उत्तम नहीं माना जाएगा। (UPBoardSolutions.com) उत्तम गृह-सज्जा से औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता तथा आधुनिकता के गुणों की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
![]()
(3) उपयोगिता-गृह-सज्जा का एक मूल सिद्धान्त है–गृह-सज्जा का उपयोगी होना। भवननिर्माण के सन्दर्भ में एक अमेरिकी वास्तुकार लुई सलीवन का कथन है कि भवन की आकृति को
व्यावहारिक होना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार गृह-सज्जा को उपयोगी होना चाहिए। निरर्थक एवं कोरी सजावट उचित नहीं होती। इस सिद्धान्त के अनुसार घर का निर्माण तथा उसकी सज्जा वैज्ञानिक तथा एक सुनिश्चित दृष्टिकोण के अनुसार होनी चाहिए।
जिस प्रकार किसी यन्त्र या उपकरण से हम अधिकतम कार्यशीलता की अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार घर से भी अधिकतम सुविधा तथा उपयोगिता की अपेक्षा की जाती है। यह तभी सम्भव है, जब कि गृह-सज्जा में उपयोगिता के सिद्धान्त का समावेश हो। इस सिद्धान्त को महत्त्व देते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि गृह-सज्जा के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं एवं उपकरणों को चुना जाए जो उपयोगी हों। जो वस्तुएँ या उपकरण उपयोगी नहीं होते, उन्हें एकत्र करना उचित नहीं माना जाता। इस मान्यता के अनसार घर के प्रत्येक कक्ष में उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं को रखा जाता है। गृह-सज्जा के लिए अपनाई जाने (UPBoardSolutions.com) वाली प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता की भली – भाँति परख कर लेनी चाहिए।
उदाहरण के लिए-सोफा एवं सोफे का कवर ऐसा । होना चाहिए, जो अधिक मजबूत, टिकाऊ एवं सुविधाजनक हो। अनावश्यक मीनाकारी, कढ़ाई एवं कृत्रिम सुन्दरता को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार परदे तथा कालीन भी मजबूत एवं पक्के रंग के होने चाहिए। जो वस्तुएँ किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करती हों, उन्हें गृह-सज्जा में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि उपयोगिता के सिद्धान्त को मानते हुए गृह-सज्जा में सुन्दरता एवं आकर्षकता के तत्त्व की पूर्ण अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में सुन्दरता तथा उपयोगिता, कला तथा विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। गृह-सज्जा में समन्वयात्मक सिद्धान्त को ही अपनाया जाना चाहिए, जिसमें सुन्दरता, अभिव्यक्ति तथा उपयोगिता का समुचित समावेश हो।
प्रश्न 3
गृह-सज्जा के कलात्मक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
या
सजावट के मूलभूत आधार क्या हैं? सजावट में रंग-व्यवस्था का क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिए।
या गृह-सज्जा के मूलभूत कलात्मक सिद्धान्त कौन-से हैं? किन्हीं दो सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
गृह-सज्जा के कलात्मक सिद्धान्त (आधार) कला किसी सुन्दर विषय-वस्तु के प्रति मनुष्य की अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसके उदाहरण हैं–प्रकृति, संगीत, गीत, मूर्ति निर्माण, चित्रकला, सुन्दर-सुन्दर भवनो के निर्माण इत्यादि। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कला का अपना अलग महत्त्व है। कला के निर्माण के चार मुख्य तत्त्व हैं-रेखाएँ, आकार, बनावट की विधियाँ तथा रंग। गृह-सज्जा में कला के इन मूल तत्त्वों के आधार पर कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। गृह-सज्जा के प्रमुख मूलभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
- समानुपात,
- लय,
- सबलता या क्रम,
- सन्तुलन तथा
- अनुकूलन।।
![]()
(1) समानुपात-गृह-सज्जा का एक प्रमुख सिद्धान्त है-समानुपात का सिद्धान्त। कमरे में फर्नीचर व्यवस्थित करने, पुष्प एवं चित्र लगाने, दीवारों की सजावट इत्यादि में वस्तु एवं पृष्ठभूमि में समानुपात का ध्यान रखना चाहिए। समानुपात डिजाइन बनाने का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसमें किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के तुलनात्मक सम्बन्धों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए—मकान के कमरों व उनके (UPBoardSolutions.com) दरवाजो एवं खिड़कियों की लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई समानुपात के नियमों के अनुसार रखने पर उनकी शोभा बढ़ जाती है। एक बड़े कमरे में उसी अनुपात में रखा बड़ी सोफा तथा उसके पीछे दीवार पर समानुपात मे लगा बड़े आकार का चित्र अधिक अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार फूलदान व फूलों में नियमित समानुपात रखने पर पुष्प-सज्जा अधिक आकर्षक प्रतीत होती है।
(2) लय-आकृतियों, नापों, रेखाओं तथा रंगों के सम्बन्ध को लय कहते हैं। इसका गति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसमें रेखाओं, आकृतियों व रंगों आदि का प्रयोग बार-बार एक निश्चित क्रम में किया जाता है। घर की सजावट में प्रत्येक स्थान पर लय का होना आवश्यक है।
(3) सबलता या क्रम-दृश्य-कला; जैसे—चित्र, मूर्ति, कशीदाकारी, आदि; में कुछ अंश प्रमुख होते हैं। ये आकर्षण बिन्दु होते हैं तथा सबल अंश कहलाते हैं। सबलता का यह सिद्धान्त गृह-सज्जा में
भी प्रयुक्त होता है। घर के किसी भी कमरे में खिड़की के परदे, अच्छे चित्र, दरी-कालीन आदि में से कोई भी एक आकर्षण का केन्द्र हो सकता है, परन्तु कमरे की सजावट में आकर्षण बिन्दु एक अथवा . दो से अधिक नहीं होने चाहिए।
(4) सन्तुलन--विभिन्न आकारों, डिजाइनों व रंगों इत्यादि के मध्य व्यवस्थित सम्बन्ध सन्तुलन कहलाता है। सन्तुलन दो प्रकार का होता है–
(अ) औपचारिक-यह नियमित सन्तुलन होता है। इसमें प्रमुख केन्द्रबिन्दु के दोनों ओर समान भार व समान आकृतियों की वस्तुओं को समान दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है।
(ब) अनौपचारिक–यह अनियमित सन्तुलन अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसमें किसी असमान भार वाली वस्तुओं को केन्द्र-बिन्दु के दोनों ओर असमान दूरियों पर व्यवस्थित किया जाता है।
![]()
(5) अनुकूलन-जब वस्तुओं में पर्याप्त आपसी समानता दिखाई देती है तो इसे अनुकूलन अथवा अनुरूपता कहते हैं। गृह-सज्जा में अनुकूलता के सिद्धान्त को कला के चारों प्रमुख तत्त्वों; रेखा, आकार, बनावट तथा रंग; के प्रयोग में लागू कर सकते हैं।
| गृह-सज्जा में रंग व्यवस्था का महत्त्व उचित रंग कमरे की शोभा को (UPBoardSolutions.com) जहाँ चार-चाँद लगा सकते हैं, वहीं अनुचित रंग उसको भद्दा भी बना सकते हैं। बढ़िया कपड़े का परदा कलात्मक दृष्टि से किसी काम का नहीं यदि उसका रंग कमरे के अनुकूल नहीं बैठता। कभी-कभी साधारण-सी वस्तु से उपयुक्त रंग के कारण कमरे की सज्जा का प्रभाव कहीं अधिक बढ़ जाता है।
प्रश्न 4
गृह को सुसज्जित करने के क्या-क्या साधन हैं? सविस्तार वर्णन कीजिए। 2018, 10, 11]
या
घर के पर्दे एवं चित्रों का चुनाव किस प्रकार करेंगी? समझाइए। 2011]
फूलों तथा चित्रों का दैनिक जीवन में क्या महत्त्व है? 2008, 11, 12]
या
घर की आन्तरिक सज्जा से आप क्या समझती हैं? गृह-सज्जा के लिए उपयोगी साधनों के बारे में लिखिए। 2007, 12, 14]
फूलों एवं चित्रों का गृह-सज्जा में महत्त्व लिखिए। [2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17}
घर की सजावट में फर्नीचर का क्या महत्त्व है? (2015
या
गृह-सज्जा में पदें व पुष्प का क्या महत्त्व है? 2018
उत्तर:
(संकेत-घर की आन्तरिक सज्जा के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 का आरम्भिक भाग देखें। गृह-सज्जा के साधन घर की सजावट के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं
(1) फर्नीचर-कुर्सियां, मेजें, डेस्कें, सोफे, पलंग, तख्त, दीवाने, चौकियाँ, अलमारियाँ, रैके, शैल्फ इत्यादि प्रमुख प्रकार के फर्नीचर हैं। प्रायः फर्नीचर लकड़ी, स्टील व ऐलुमिनियम के बनते हैं। लकड़ी के फर्नीचर अधिक मूल्यवान होते हैं। फर्नीचर (UPBoardSolutions.com) खरीदते समय इसकी आवश्यकता, टिकाऊपन व अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। सजावट के लिए फर्नीचर खरीदते समय घर में इसके लिए उपलब्ध स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। महानगरों में प्रायः स्थान बचाऊ फर्नीचर; जैसे–फोल्डिग कुर्सियाँ, मेज व पलंग आदि; का प्रयोग किया जाता है।
(2) परदे-खिड़कियों एवं दरवाजों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य के रंग-बिरंगे परदे लगाए जाते हैं। परदे का उपयोग गोपनीयता के लिए तथा वायु, प्रकाश, गर्मी एवं ठण्ड से बचाव केलिए किया जाता है। परदे कमरे को सुन्दर एवं आकर्षक बनाते हैं; अत: घर के विभिन्न कमरों के लिए परदों के डिजाइन व रंगों का चयन करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। परदे घर की सजावट का महत्त्वपूर्ण साधन हैं।
![]()
(3) दरी एवं कालीन-इनका उपयोग ठण्डे प्रदेशों में ठण्ड से बचाव के लिए तथा कच्चे एवं सीमेण्ट के फर्श को ढकने के लिए होता है। आजकल दरी के स्थान पर जूट की बनी चटाई प्रयोग में
लाई जाती हैं। कालीन एक मूल्यवान वस्तु है; अत: इनको खरीदते समय अपनी आर्थिक क्षमता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कालीन का नाप, रंग व डिजाइत परदों के डिजाइन व रंग से समन्वित एवं सन्तुलित होना चाहिए।
(4) चित्र एवं मूर्तियाँ-घर की सजावट के लिए यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला साधन है। तैलचित्र हों अथवा पेन्टिग्स, विभिन्न कमरों को सजाते समय इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए-ड्राइंग-रूम में महापुरुषों के चित्र तथा शयन-कक्ष में शृंगारिक चित्रों को लगाना उचित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन-सा कमरा किस उपयोग का है। उसमें उसी के अनुरूप चित्र लगाने चाहिए। मूर्तियों एवं खिलौनों का उपयोग भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
(5) पुष्प-सज्जा-फूल एवं साज-सज्जा वाले पौधे भी चित्र एवं मूर्तियों के समान सजावट का प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा घर की बाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रकार की सजावट की जा सकती है। उदाहरण के लिए भूमि अथवा गमलों में लगे फूल वाले तथा साज-सज्जा वाले पौधे घर की बाह्य सजावट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा फूलों को फूलदान व अन्य पात्रों में लगाकर घर की
आन्तरिक सजावट की जाती है। घर की सजावट में फूलों को विविध प्रकार से उपयोग में लाया जाता। है। उदाहरण के लिए—इन्हें ड्राइंग-रूम में, पढ़ने के कमरे अर्थात् स्टडी में, किताबों की शेल्फ पर रखे फूलदान में तथा भोजन-कक्ष में भोजन की मेज आदि पर सजाया जाता है।
![]()
प्रश्न 5
बैठक (ड्राइंग-रूम) से क्या आशय है? घर के इस कमरे के महत्त्व एवं सजावट की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। घर में बैठक का क्या महत्त्व है? अपने घर की बैठक को आप किस प्रकार सजाएँगी? स्पष्ट कीजिए। [2018]
या
बैठक की सजावट के उपकरण तथा विधि लिखिए।
या
बैठक की सजावट में किन-किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? [2011, 12, 13, 14, 16]
उत्तर:
बैठक (ड्राइंग-रूम) से आशय
प्रत्येक व्यक्ति के घर पर किसी-न-किसी प्रयोजन से समय-समय पर कुछ लोग मिलने के लिए अवश्य आया करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के साथ तो घनिष्ठ मित्रता के सम्बन्ध होते हैं तथा कुछ के साथ केवल औपचारिक सम्बन्ध ही होते हैं। औपचारिक सम्बन्ध वाले व्यक्तियों को हम हर समय अपने शयन-कक्ष में या भोजन के कमरे में नहीं बैठा सकते। स्पष्ट है कि इस प्रकार के आगन्तुकों के स्वागत एवं बैठाने के लिए एक कमरा अलग से होना (UPBoardSolutions.com) चाहिए। इसी कमरे को बैठक या ड्राइंग रूम कहा जाता है। आजकल प्रायः सभी घरों में ड्राइंग-रूम बनाने का प्रचलन है। ड्राइंग-रूम में प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्ति को बैठाया जाता है। सामान्य रूप से यह कमरा घर के मुख्य द्वार के निकट ही बनाया जाता है, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधापूर्वक वहीं बैठाया जा सके। बैठक का महत्त्व ड्राइंग-रूम अथवा बैठक प्रत्येक घर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि
- इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं अतिथियों का स्वागत किया जाता है। अतः इस कमरे की सजावट अन्य कमरों से अधिक सुरुचिपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होती है।
- यह घर के मुख्य द्वार का निकटतम कमरा होता है। घर के अन्य कमरों में चाहे सजावट न हो, परन्तु ड्राइंग-रूम को सदैव सजावट द्वारा सुरुचिपूर्ण बनाया जाता है।
- आगन्तुक प्रायः इसी कमरे में बैठते हैं; अत: इससे घर की गोपनीयता बनी रहती है।
- बैठक की साज-सज्जा घर के रहन-सहन के स्तर एवं संस्कृति की परिचायक होती है।
- बैठक की सजावट-मुख्य शैलियों द्वारा पूरे घर में बैठक को रहन-सहन के स्तर के अनुरूप पूर्ण सूझ-बूझ के साथ सजाया जाता है।
सजावट करने की विभिन्न विधियों को तीन प्रमुख शैलियों में विभाजित किया जाता है-
- परम्परागत देशी शैली,
- विदेशी शैली तथा
- मिश्रित शैली।
(1) सजावट की परम्परागत देशी शैली-यह मूल रूप से भारतीय शैली की सजावट की पद्धति है। इसमें एक तख्त या दीवान बिछाया जाता है जिस पर एक सुन्दर चादर बिछाई जाती है। दीवान पर मसनद या गाव तकिए रखे जाते हैं। बैठक के आकार एवं उपलब्ध स्थान के अनुसार मूढ़े भी रखे जाते हैं। मूढ़ों पर आकर्षक गद्दियाँ रखी जाती हैं। बैठक के फर्श पर दरी बिछाई जाती है। कमरे के केन्द्रीय भाग में दरी पर कालीन बिछाया जाता है। कमरे के सिरे पर एक सुन्दर अलमारी रखी जाती है। इस पर रेडियो अथवा टी० वी० भी रखा जा सकता है। इसके अन्य खानों में सजावट की वस्तुएँ अथवा उच्चकोटि की पुस्तकें रखी जा सकती हैं। दीवारों की सजावट आकर्षक चित्रों एवं अन्य सामग्रियों द्वारा की जाती है।
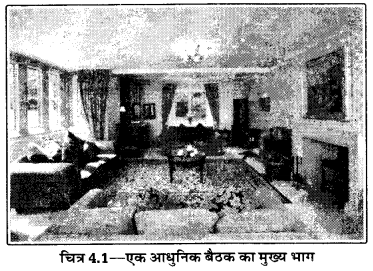
(2) सजावट की विदेशी शैली—इस शैली में दीवान व मूढ़ों के स्थान पर सोफा लगाया जाता है। कमरे के आकार एवं उपलब्ध स्थान के आधार पर सोफे संख्या में दो अथवा अधिक भी हो सकते हैं। फर्श पर आवश्यकतानुसार दरी व कालीन बिछाए जा सकते हैं। प्रत्येक सोफे के सामने एक सेण्टर-टेबल रखी जा सकती है। यह सनमाइका या काँच की। हो सकती है, अन्यथा इस पर कपड़े या प्लास्टिक का सुन्दर कवर भी भाग बिछाया जा सकता है। दो छोटी मेजें भी रखी जा सकती हैं, जिन्हें साइड टेबिल कहा जाता है। इन पर ऐश-ट्रे आदि रखी जा सकती हैं। कमरे में एक ओर एक आकर्षक कैबिनेट में टी० वी० रखा जा सकता है। दीवारों (UPBoardSolutions.com) पर साधारण अथवा तैल-चित्र सजाए जा सकते हैं। दरवाजों एवं खिड़कियों पर आकर्षक परदे लगाए जा सकते हैं। परदों, दीवारों व अन्य सामग्रियों का चयन करते समय विरोधी एवं सहयोगी रंगों का ध्यान रखना चाहिए। रंगों का उपयुक्त चुनाव सजावट के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है।
![]()
(3) सजावट की मिश्रित शैली– इसमें देशी एवं विदेशी दोनों शैलियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए-दीवान तथा सोफा दोनों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कुर्सियाँ तथा मूढ़े दोनों ही रखे जाते हैं। यद्यपि इस शैली में कोई मौलिकता नहीं होती फिर भी यह शैली”अधिक लोकप्रिय एवं सुविधाजनक है।
प्रश्न 6
खाने के कमरे (डाइनिंग रूम) की सजावट आप कैसे करना पसन्द करेंगी और क्यों?
देशी तथा विदेशी शैली के अनुसार खाने के कमरे (भोजन-कक्ष) की साज-सज्जा आप किस प्रकार करेंगी?
भारतीय तथा पाश्चात्य शैली के भोजन-कक्ष में क्या अन्तर है? विस्तारपूर्वक लिखिए। भोजन-कक्ष की सजावट की विधि लिखिए। [2013]
उत्तर:
मानव जीवन में भोजन ग्रहण करने का विशेष महत्त्व है। व्यक्ति भोजन जुटाने के लिए ही अनेक परेशानियाँ उठाता है। एक समय था, जब लोग पाकशाला या रसोईघर में ही बैठकर शान्त भाव से भोजन ग्रहण किया करते थे। उस समय जीवन सादा एवं सरल तथा कर्म व्यस्त था। आज जीवन बदल गया है। आज पाकशाला में बैठकर भोजन ग्रहण करने की सुविधा नहीं है। आधुनिक घरों में प्रायः रसोईघर काफी छोटे होते हैं; अत: वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जीवन व्यस्त होने के कारण अनेक बार जूते-मोजे तथा पैंट-कोट पहने हुए ही भोजन ग्रहण करना पड़ता है। इस दशा में रसोईघर में बैठकर भोजन (UPBoardSolutions.com) नहीं किया जा सकता। इन समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आजकल प्रायः सभी घरों में भोजन को अलग कमरा बनाया जाता है। इस कमरे को ही भोजन का कमरा’ या ‘डाइनिंग रूम’ (Dining room) कहा जाता है।
खाने के कमरे की सजावट
खाने के कमरे की सजावट में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है-सफाई। खाने का कमरा हर प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए। इस कमरे में संवातन तथा प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। खाने के कमरे की सजावट की मुख्य शैलियों या विधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवर्णित है
(1) परम्परागत देशी शैली-भारतीय शैली में भोजन ग्रहण करने के लिए चौकी, पटरी अथवा आसन का उपयोग किया जाता है। देशी शैली में भोजन-कक्ष में सुविधाजनक चौकी, पटरी अथवा आसन की व्यवस्था की जाती है। चौकियों पर सुन्दर-सुन्दर मेजपोश बिछाए जाते हैं। भोजन करते समय रेक्सिन अथवा प्लास्टिक के कपड़े चौकियों पर बिछाए जाते हैं। ये सुन्दर तथा आकर्षक डिजाइनों व रंगों के होते हैं और भोजन गिरने पर स्थायी रूप से गन्दे नहीं होते। दीवारों की सजावट बैठक के कमरे की अपेक्षा साधारण होती है। भोजन कक्ष में रेफ्रिजेरेटर या पानी रखने का कोई अन्य साधन भी रखा जाता है। भोजन-कक्ष प्रायः रसोईघर से जुड़ा होता है, ताकि भोजन लाने-ले-जाने की सुविधा रहे। देशी शैली में भोजन थालियों एवं कटोरियों में परोसा जाता है; अत: भोजन-कक्ष में बर्तन रखने के लिए अलमारी भी रखी जा सकती है।
(2) विदेशी शैली—इस शैली में भोजन-कक्ष में एक बड़ी मेज (डाइनिंग टेबल) तथा इसके चारो ओर बिना हत्थे वाली चार अथवा छ: कुर्सियाँ (डाइनिंग चेयर्स) लगाई जाती हैं। डाइनिंग टेबल की ऊपरी सतह पर रेक्सिन, शीशा अथवा सनमाइका लगी होती है। इसका लाभ यह होता है कि भोजन इत्यादि गिरने पर डाइनिंग टेबल को सरलतापूर्वक साफ किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर अथवा पानी के किसी अन्य साधन की व्यवस्था भी भोजन-कक्ष में ही की जानी चाहिए।
![]()
(3) भोजन-कक्ष निश्चित रूप से रसोईघर से जुड़ा होना चाहिए। भोजन-कक्ष में एक ओर हाथ-मुँह धोने के लिए एक वाशबेसिन लगा होना चाहिए। इसमें साबुन व स्वच्छ तौलिए की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन-कक्ष के दरवाजे एवं खिड़कियों पर साधारण, परन्तु स्वच्छ एवं आकर्षक परदे लगे होने चाहिए। भोजन-कक्ष की खिड़कियों पर लोहे के तार की जाली लगानी आवश्यक है। यह भोजन-कक्ष में मक्खियों को प्रवेश नहीं करने देती। दीवारों पर अच्छे-अच्छे चित्र व डाइनिंग टेबल पर पुष्पों से सज्जित फूलदान भोजन प्राप्त करने वालों के मन को प्रसन्न करते हैं।
प्रश्न 7
शयन-कक्ष की सजावट का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए।
या
घर में शयन-कक्ष कहाँ होना चाहिए तथा उसकी सजावट में किन बातों का ध्यान रखना आप आवश्यक समझती हैं? स्पष्ट कीजिए।
या
शयन-कक्ष की सजावट की वस्तुओं की सूची बनाइए। [2013
उत्तर:
घर में शयन-कक्ष विश्राम के लिए नींद सर्वाधिक आवश्यक है। नींद के लिए शान्त एवं एकान्त वातावरण आवश्यक होता है; अतः सोने के लिए अलग से एक कमरा निर्धारित किया जाता है। इस कमरे को ही ‘शयन- कक्ष’ कहा जाता है। मकान में शयन-कक्ष के लिए ऐसे कमरे का चुनाव करना चाहिए जहाँ अधिक शोर की सम्भावना न हो तथा जिस कमरे में से होकर आना-जाना आवश्यक न हो। जहाँ तक सम्भव हो बाहरी द्वार से पीछे हटकर ही शयन-कक्ष होना चाहिए। शयन-कक्ष हवादार एवं साफ होना चाहिए।
शयन-कक्ष की सजावट में ध्यान रखने योग्य बातें
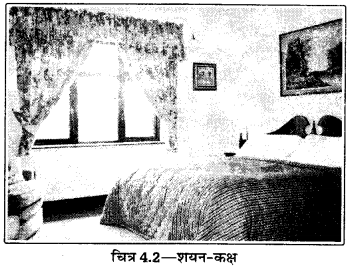
शयन-कक्ष की सजावट विशेष रुचिपूर्वक करनी चाहिए। शयन-कक्ष में सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण वस्तु है—पलंग। पलंग अधिक-से-अधिक आरामदायक होना चाहिए। पलंग पर अच्छी-से-अच्छी चादर बिछाई जानी । चाहिए। पलंग के अतिरिक्त शयन-कक्ष में एक (UPBoardSolutions.com) या दो साइड-टेबिल भी होने चाहिए। इन पर पानी-दूध आदि रखे जा सकते हैं। शयन-कक्ष में ही श्रृंगार-मेज भी रखी जाती है। श्रृंगार-मेज के दर्पण पर अच्छे कपड़े का कवर डाला जा सकता है।
![]()
शयन-कक्ष को सुसज्जित करने के लिए गहरे रंग के मोटे कपड़े के परदे लगाए जा सकते हैं। इससे एकान्त प्राप्त होता है तथा बाहरी धूप, चौंध आदि से भी बचा जा सकता है। शयन-कक्ष में अन्य प्रकाश के अतिरिक्त नाइट बल्ब अवश्य लगाया जाता है। शयन-कक्ष को सुसज्जित करने के लिए कुछ कलाकृतियाँ भी रखी जा सकती हैं। यदि इस कक्ष में केवल पति-पत्नी को ही सोना हो, तो कुछ शृंगारिक चित्र एवं मूर्तियाँ भी रखी जा सकती हैं। शयन-कक्ष की सजावट में कमरे में सोने वालों की रुचि का सर्वाधिक महत्त्व होता है। इसमें दिखावट या प्रदर्शन के दृष्टिकोण से सज्जा नहीं की जाती। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शयन-कक्ष की सजावट की प्रमुख विशेषता है-विश्राम में सहायक होना।
प्रश्न 8
रसोईघर की सजावट आप किस प्रकार करेंगी? समझाइए।
उत्तर:
रसोईघर प्रत्येक घर का एक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से परिवार के सभी सदस्यों एवं अतिथियों को भोजन सुलभ होता है। अत: इसका स्वच्छ तथा कीटाणु एवं कीट-पतंगों रहित रहना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक घर में गृहिणी प्रायः रसोईघर की संचालिका होती है। उसे परिवार के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी करने होते हैं। इसलिए रसोईघर का गृहिणी के लिए सुविधाजनक होना अत्यावश्यक है। धुओं व गन्दे पानी के निकलने की (UPBoardSolutions.com) व्यवस्था, पानी, प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था, बर्तन एवं खाद्य पदार्थ रखने की व्यवस्था तथा व्यवस्थित प्रकार से रखे हुए यन्त्र एवं उपकरण गृहिणी की कार्यकुशलता में अपार वृद्धि करते हैं। गृहिणी रसोईघर की सजावट प्राय: निम्नलिखित शैलियों द्वारा करती है
(1) परम्परागत देशी शैली–इस शैली में व्यवस्थित रसोईघर में गृहिणी भोजन बनाना, बर्तन धोना आदि सभी कार्य बैठकर करती है। इसमें एक ओर चूल्हा अथवा अँगीठी होती है जिसका धुआँ बाहर जाने के लिए रसोईघर की छत में व्यवस्था होती है। रसोईघर में पानी की व्यवस्था के लिए एक नल लगा होता है। एक सुव्यवस्थितं एवं सुसज्जित रसोईघर में नल के पास ही एक अलमारी अथवा रैक होती है, ताकि साफ करने के बाद बर्तन इसमें सुविधापूर्वक रखे जा सकें। अलमारी में सभी खाद्य पदार्थ एवं मिर्च-मसाले अलग-अलग बन्द डिब्बों में उनके नाम की चिटें लगाकर रखे जाते हैं। रसोईघर से गन्दे पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
(2) विदेशी शैली–इस शैली में व्यवस्थित रसोईघर में गृहिणी भोजन बनाना, बर्तन साफ करना आदि सभी कार्य खड़े होकर करती है। इसके लिए रसोईघर का आकार थोड़ा बड़ा तथा उपलब्ध स्थान अधिक होना चाहिए। रसोईघर के दरवाजे के सामने व दोनों ओर खड़े होकर कार्य करने योग्य ऊँचे सीमेण्ट के चबूतरे अथवा टेबल लगाए जाते हैं। इस प्रकार बने ऊँचे आधार पर गैस का चूल्हा रखा जाता है तथा आधार के नीचे गैस-सिलेण्डर रखने की व्यवस्था होती है। दीवार पर लगे रैक पर चिमटा, सन्डासी, कद्दूकस इत्यादि रखे होते हैं।
दोनों ओर लगी अलमारियों में बर्तन तथा नामांकित खाद्य-पदार्थ एवं मिर्च-मसाले रखे जाते हैं। रसोईघर में एक ओर बर्तन इत्यादि धोने के लिए सिंक लगा होता है। सिंक के पास कूड़ादान, झाड़न व झाड़ रखी होती है। विदेशी शैली के अनुसार व्यवस्थित रसोईघर में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं
- यह सजावट की एक आधुनिक शैली है
- सफाई में सुविधा के कारण रसोईघर स्वच्छ व सुन्दर बना रहता है।
- खड़े रहकर कार्य करने की सुविधा के कारण गृहिणी को थकान कम होती है।
- गृहिणी के वस्त्र न तो मुड़ते-सिकुड़ते हैं और न ही गन्दे होते हैं।
![]()
प्रश्न 9
फूलों से सजावट किस प्रकार की जाती है? इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? या गृह-सज्जा में पुष्प-सज्जा के महत्त्व को लिखिए।[2011]
उत्तर:
पुष्प-सज्जा के प्रकार
फूलों द्वारा घर की सजावट निम्नलिखित दो प्रकार से की जा सकती है
(1) बाह्य सजावट-घर के आगे और पीछे दोनों ओर खाली भूमि में पुष्प वाले पौधे उगाए जा सकते हैं। पुष्प वाले पौधों के अतिरिक्त साज-सज्जा वाले पौधे; जैसे-कैक्टस, क्रोटन, कोलियस, रबर-प्लाण्ट इत्यादि; रिक्त भूमि व गमलों में लगाए जा सकते हैं। दीवारों (UPBoardSolutions.com) एवं खिड़कियों आदि से लगी हुई अनेक प्रकार की आकर्षक बेलें; जैसे-बोगेनवेलिया, रेलवे-क्रीपर, सतावर आदि; उगाई जा सकती हैं।
(2) आन्तरिक सजावट-घर के अन्दर की सजावट बोतलों, गिलासों, डिब्बों और विशेष रूप से विभिन्न आकार एवं प्रकार के फूलदानों में पुष्प लगाकर की जाती है। पुष्प युक्त पौधों को भी गमलों सहित कभी-कभी ड्राइंग-रूम में रख दिया जाता है।
पुष्प-सज्जा की विभिन्न शैलियाँ
- परम्परागत देशी शैली–इससे विभिन्न रंगों, आकार एवं प्रकार के पुष्पों का गुलदस्ता बनाकर किसी पात्र अथवा फूलदान में लगाया जाता है। इसमें फूलों व फूलदान के रंगों व आकार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
- विदेशी शैली—इसमें पुष्पों को विदेशी ढंग से सजाया जाता है। इस प्रकार की पुष्प-व्यवस्था में अनियमित सन्तुलन पर बल दिया जाता है। इसमें सन्तुलन की व्यवस्था 3, 5, 7, 9 फूलों से की जाती है और तीन टहनियों का प्रयोग होता है। पुष्प-सज्जा की इस शैली को इकेबाना कहा जाता है तथा यह मूल रूप से एक जापानी शैली है।।
- आधुनिक शैली—यह उपर्युक्त दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इस शैली के अन्तर्गत पुष्पों को परम्परागत शैली के अनुसार गुलदस्ते के रूप में न बाँधकर पिन होल्डर की सहायता से पात्रे में लगाया जाता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- फूलों को सदैव प्रात:काल अथवा सूर्यास्त होने पर काटना चाहिए।
- फूलों को काटकर पानी से नम बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल अधिक समय तक ताजा रहते हैं।
- फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। इन्हें कैंची या छुरी से काटना चाहिए।
- फूलदान में पानी इतना रहना चाहिए कि फूलों की टहनियाँ इसमें डूबी रहें।
- फूलदान अथवा अन्य पुष्प पात्रों को समय-समय पर साफ करके चमकाना चाहिए।
- फूलों को उनकी पत्तियों के साथ फूलदान में लगाना चाहिए। इससे स्वाभाविकता दिखाई पड़ती है।
- फूलों को मौसम के अनुसार सजाना चाहिए।
- पानी में नमक डालने से पुष्प देर से मुरझाते हैं।
![]()
गृह–सज्जा में पुष्प-सज्जा का महत्त्व गृह-सज्जा के सन्दर्भ में पुष्प-सज्जा का विशेष महत्त्व है। फूल सुन्दरता के प्रतीक तथा गृह-सज्जा के प्रकृति-प्रदत्त साधन हैं। फूलों का सौन्दर्य बच्चों, बूढ़ों तथा स्त्री-पुरुष सभी के लिए विशेष आकर्षक होता है। एक कवि बिशप कॉक्स ने कहा है, “पुष्प ऐसी भाषा है, जिसे एक बच्चा भी समझता है।” फूलों से वातावरण में ताजगी, उल्लास एवं उत्साह का संचार होता है। फूल वातावरण की नीरसता को (UPBoardSolutions.com) समाप्त करते हैं। फूल व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। फूलों के इन बहुपक्षीय लाभों एवं अद्वितीय सौन्दर्य के कारण गृह-सज्जा में इन्हें विशेष महत्त्व दिया गया है। रट के शब्दों में, “एक चिन्तित और दु:खी व्यक्ति को पुष्प-व्यवस्था से अपने दुःखों से छुटकारा तथा तसल्ली मिलती है।”
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
‘घर की सफाई तथा ‘गृह-सज्जा’ के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
‘घर की सफाई’ तथा ‘गृह-सज्जा’ का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। गृह-सज्जा के लिए अनिवार्य है कि घर में सफाई भी हो। सफाई से आशय है-गन्दगी का अभाव, जबकि सजावट का अर्थ है-घर की वस्तुओं की सुन्दर एवं कलात्मक व्यवस्था। सजावट के अभाव में भी घर की सफाई रह सकती है, परन्तु घर की सफाई के अभाव में घर को सुसज्जित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सजावट के अभाव में सफाई रह सकती है, परन्तु सफाई के अभाव में सजावट सम्भव नहीं है।
प्रश्न 2
घर में बच्चों के कमरे की उचित सजावट आप किस प्रकार करेंगी? या स्कूल जाने वाले बालक के कमरे की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे? [2011]
उत्तर:
पढ़ने वाले बच्चों का कमरा खुला, हवादार, प्रकाशमय तथा गृहिणी के कमरे के पास होता है। यह बच्चों के अध्ययन के लिए उपयुक्त रहता है। इस कमरे की सजावट एवं व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है
- बच्चों के लिए अलग-अलग आवश्यक ऊँचाई की डेस्क व कुर्सियों की व्यवस्था।
- बिजली के बल्ब, ट्यूब व टेबल लैम्प द्वारा उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था।
- समय देखने के लिए तथा सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी।
- दिनांक देखने के लिए कमरे में एक कैलेण्डर होना चाहिए।
- कमरे के दरवाजे और खिड़कियों आदि पर उचित रंग के परदे होने चाहिए।
- दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र तथा बच्चों की रुचि के अनुसार प्रसिद्ध खिलाड़ियों के चित्र होने चाहिए।
- पुस्तकें तथा स्कूल बैग रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था।
- कपड़े रखने की अलमारी की व्यवस्था।
- सोने के लिए पलंग व बिस्तर आदि की व्यवस्था।
![]()
प्रश्न 3
टिप्पणी लिखिए-घर के बरामदे का महत्त्व एवं सजावट।
उत्तर:
भारतीय घरों में बरामदे का अधिक उपयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु में सुबह और शाम तथा वर्षा ऋतु में बरामदे में बैठना बड़ा रुचिकर लगता है। सर्दियों में दिन के समय कमरे बहुत ठण्डे रहते हैं। अत: बरामदा धूप और प्रकाश के कारण अधिक भाता है। बरामदा एक बहुउद्देशीय कक्ष या अनौपचारिक बैठक का काम करता है। बहुधा आगन्तुकों एवं मित्र वर्ग के साथ गप्पे मारने का भी यही स्थान होता है। इसीलिए बेंत को हल्का फर्नीचर व दो-चार गमले बरामदे में अवश्य लगाने चाहिए। बरामदे में क्रोटन, पाम, डिफनबेकिया तथा मनी-प्लाण्टे के गमले भी रखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त दीवार पर एक-दो चित्र भी लगाए जा सकते हैं।
प्रश्न 4:
टिप्पणी लिखिए-संयुक्त स्नान-गृह एवं शौचालय।
उत्तर:
वर्तमान भारतीय जीवन में पाश्चात्य प्रभाव एवं प्रचलन क्रमशः बढ़ रहे हैं। पाश्चात्य प्रचलन के ही अनुसार अब हमारे देश में भी स्नान-गृह एवं शौचालय संयुक्त रूप से बनाए जाने लगे हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही कमरे में नहाने की व्यवस्था के साथ-ही-साथ शौच का भी प्रावधान होता है। इस व्यवस्था के अनुसार कमरे में एक ओर कमोड अर्थात् शौच का स्थान तथा दूसरी ओर नहाने का स्थान होता है। इस प्रकार के स्नान–गृह एवं शौचालय सामान्य रूप से शयन-कक्ष के साथ जुड़े रहते हैं।
इन्हें अत्यधिक स्वच्छ रखना अनिवार्य होता है। अतः यदि घर में फ्लश सिस्टम का प्रावधान न हो तो यह व्यवस्था उत्तम नहीं मानी जाती। वैसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के संयुक्त स्नान-गृह एवं शौचालय काफी सुविधाजनक होते हैं। व्यक्ति एक साथ ही शौच एवं स्नान (UPBoardSolutions.com) कार्य से निवृत हो सकता है। इस प्रावधान के होने की स्थिति में रात्रि में अथवा ठण्ड के समय व्यक्ति को अपने शयन-कक्ष से दूर नहीं जाना पड़ता।
प्रश्न 5
घर के लिए फर्नीचर खरीदते समय मुख्य रूप से किन-किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? [2012, 13, 14, 16, 17]
उत्तर:
फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें फर्नीचर आजकल काफी महँगा मिलता है; अत: रोज-रोज फर्नीचर नहीं खरीदा जाता। कपड़ों की तरह फर्नीचर रोज-रोज बदला भी नहीं जा सकता। अत: फर्नीचर खरीदते समय विशेष सूझ-बूझ एवं समझदारी से काम लिया जाना चाहिए। फर्नीचर खरीदते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए-
(1) सर्वप्रथम यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल उपयोगी फर्नीचर ही खरीदना चाहिए। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए ही या स्थान भरने के लिए ही फर्नीचर खरीदते रहते हैं। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है।
(2) दूसरी बात यह है कि वही फर्नीचर खरीदना चाहिए, जो आपके घर के अनुरूप हो अर्थात् जिस स्तर एवं प्रकार का मकान हो, उसी प्रकार का फर्नीचर खरीदना चाहिए। यदि आपका कमरा छोटा हो तो फर्नीचर भी छोटे साइज का ही खरीदना चाहिए।
(3) सामान्य रूप से फर्नीचर एक ही बार खरीदा जाता है; अतः फर्नीचर खरीदते समय फर्नीचर की मजबूती एवं कोटि को विशेष ध्यान रखना चाहिए। घटिया अथवा कच्ची लकड़ी का फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए।
![]()
(4) फर्नीचर की पॉलिश अथवा रंग-रोगन का भी ध्यान रखना चाहिए।
(5) सामान्य रूप से सादे डिजाइन का फर्नीचर ही लेना चाहिए। नक्काशी अथवा खुदाई वाले डिजाइन का फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे फर्नीचर की सफाई नहीं हो पाती तथा उसमें धूल आदि भी भर जाती है जिससे बाद में वह भद्दा प्रतीत होने लगता है।
(6) अधिक भारी फर्नीचर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों का समय-समय पर तबादला होता हो, उन्हें तो ऐसा भारी फर्नीचर बिल्कुल नही खरीदना चाहिए।
(7) फर्नीचर खरीदते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। (UPBoardSolutions.com) केवल देखा-देखी की भावना से अधिक महँगा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। अन्य फैशनों के ही समान फर्नीचर का फॅशन भी बदलता रहता है। अतः इस दिशा में सुगृहिणियों को सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए।
प्रश्न 6
घर के फर्नीचर की देखभाल और सफाई आप किस प्रकार करेंगी? [2010, 17] या लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल और सफाई का वर्णन संक्षेप में कीजिए। [2007, 10, 11, 12, 17]
उत्तर
फर्नीचर की देखभाल प्रत्येक घर में सुविधा और सजावट के लिए किसी-न-किसी प्रकार का फर्नीचर अवश्य होता है। परन्तु फर्नीचर गन्दा एवं अस्त-व्यस्त होगा, तो न तो उससे घर की शोभा बढ़ेगी और न ही वह किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा। यदि फर्नीचर की देखभाल एवं सफाई न की जाए, तो वह शीघ्र ही टूट-फूट जाता है तथा बेकार हो जाता है। अत: फर्नीचर की देखभाल एवं सफाई अनिवार्य है।
सफाई-साधारण घरों में अधिकांश फर्नीचर लकड़ी का होता है। इसकी सफाई निम्नलिखित ढंग से की जानी चाहिए
- लकड़ी की बनी हुई सभी वस्तुओं को नित्य साफ कपड़े अथवा नरम ब्रश से झाड़ना एवं पोछना चाहिए। कीमती फर्नीचर को साफ करने के लिए मुलायम चमड़े का प्रयोग भी किया जा सकता है। चमड़े से रगड़कर साफ करने से पॉलिश में चमक आ जाती है।
- कभी-कभी फनीचर को गीले कपड़े अथवा साबुन से भी साफ किया जा सकता है। इस प्रकार से साफ करने के बाद तुरन्त सूखे कपड़े से पोंछकर सुखा देना अनिवार्य है।
- पानी में सिरका मिलाकर, घोल से फर्नीचर को साफ किया जा सकता है।
- पुराने फर्नीचर में कुछ दरारें पड़ जाती हैं अथवा जोड़ खुल जाते हैं। इन दरारों को भरना आवश्यक होता है अन्यथा इनमें गन्दगी भरती रहती है। दरारों को भरने के लिए पोटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जा सकता है।
- समय-समय पर सामान्यतः प्रतिवर्ष फर्नीचर पर यदि रंग-रोगन अथवा पॉलिश करा दी जाए तो फर्नीचर की उम्र भी बढ़ती है तथा शोभा भी।
प्रश्न 7
प्लास्टिक के फर्नीचर की देखभाल तथा सफाई का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। [2017, 18]
उत्तर:
वर्तमान युग प्लास्टिक का युग है। अब जीवनोपयोगी अधिकांश वस्तुएँ प्लास्टिक से ही बनाई जा रही हैं। इसी श्रृंखला में प्लास्टिक के फर्नीचर का भी अत्यधिक प्रचलन हो गया है। प्लास्टिक का फर्नीचर सस्ता तथा सुविधाजनक होता है। इस फर्नीचर की देखभाल तथा सफाई प्रायः आसान होती है। सामान्य रूप से प्लास्टिक के फर्नीचर को किसी भी कपड़े से झाड़-पोंछ कर साफ किया जा सकता है। इससे उसकी धूल-मिट्टी का निवारण हो जाता है।
यदि प्लास्टिक के फर्नीचर पर चिकनाई, मैले या धब्बे लग जाएँ तो उस स्थिति में गीले कपड़े एवं साबुन द्वारा इसे सरलता से साफ किया जा सकता है। गीली सफाई के उपरान्त सूखे कपड़े से पोंछकर सुखा देना ही पर्याप्त होता है। प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई के समान देखभाल भी सरल है। प्लास्टिक के फर्नीचर को तेज धूप एवं ताप से बचाना अति आवश्यक होता है। यह ज्वलनशील भी होता है। अत: आग से इसे सदैव दूर रखना चाहिए। (UPBoardSolutions.com) इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्लास्टिक के फर्नीचर पर अधिक दबाव एवं वजन न डाला जाए।
![]()
प्रश्न 8
परदे क्यों लगाए जाते हैं? परदे खरीदते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगी? [2009, 10, 12]
गृह-सज्जा में परदों का क्या महत्त्व है? समझाइए। [2010, 11, 12]
कमरे के लिए परदे का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य चार सावधानियाँ लिखिए। [2011]
कमरे में परदे लगाने से क्या लाभ हैं? या घर में परदे क्यों लगाये जाते हैं? [2013]
उत्तर:
परदों की उपयोगिता निम्नलिखित है–
- परदे कमरों की सजावट का महत्त्वपूर्ण साधन होते हैं।
- ये तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठण्ड से बचाव करते हैं।
- परदे एकान्त (प्राइवेसी) बनाए रखने का महत्त्वपूर्ण साधन हैं।
- परदों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को भी छिपाया जा सकता है।
परदे खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं
- परदे पारिवारिक आय के अनुकूल होने चाहिए।
- परदे मोटे व टिकाऊ होने चाहिए।
- परदे खरीदते समय उनके आकार एवं माप का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- परदों के रंग व डिजाइन कमरों के रंग एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए।
- परदे धुलने पर अधिक सिकुड़ने वाले नहीं होने चाहिए।
- परदों के रंग पक्के होने चाहिए, ताकि धुलने के बाद हल्के न हो पाएँ।
प्रश्न 9
रंग-व्यवस्था से आप क्या समझती हैं? स्पष्ट कीजिए। या घर की सजावट में रंगों का महत्त्व लिखिए। [2008, 10, 12, 13, 16, 17]
उत्तर:
रंगों का परस्पर तालमेल अथवा समन्वय रंग-व्यवस्था कहलाता है। रंग-व्यवस्था के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं-
- कुछ रंग एक-दूसरे की निकटता से शोभा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें सहयोगी रंग कहते हैं; जैसे पीला व नारंगी, लाल व नारंगी, नीला व हरा तथा हरा व पीला इत्यादि।
- कुछ रंग एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं; जैसे—लाल व हरा, पीला व नीला इत्यादि।
- कुछ रंग गर्म प्रकृति के होते हैं; जैसे—लाल, नारंगी तथा पीला।
- कुछ रंग; जैसे कि हरा व नीला; ठण्डी प्रकृति के होते हैं।
- प्रकाशयुक्त कमरों को सदैव गहरे रंग से पेन्ट कराना चाहिए।
- कम प्रकाश वाले या अँधेरे कमरों को सफेद अथवा हल्के रंगों से पेन्ट कराना चाहिए।
- कुछ रंगों में सफेद रंग का टिण्ट देने से उनके आकर्षण में वृद्धि होती है। रंग-व्यवस्था का उपयुक्त ज्ञान घर की रंगों द्वारा सजावट करने के लिए अति आवश्यक है।
![]()
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1
गृह-सज्जा की प्रमुख शैलियाँ कौन-कौन सी हैं? (2013)
या
गृह-सज्जा के प्रकार बताइए। (2017)
उत्तर:
गृह-सज्जा की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं
- परम्परागत देशी शैली,
- विदेशी शैली तथा
- मिश्रित शैली।
प्रश्न 2
शयन-कक्ष एवं अध्ययन-कक्ष का स्थान कैसा होना चाहिए?
उत्तर:
दोनों के लिए स्वच्छ एवं शान्त स्थान होना चाहिए।
प्रश्न 3
गृह-सज्जा का प्रमुख साधन किसे माना जाता है?
उत्तर:
फर्नीचर को गृह-सज्जा का प्रमुख साधन माना जाता है।
प्रश्न 4
घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? [2011]
उतर:
घरेलू फर्नीचर आकर्षक होने के साथ-साथ मजबूत, टिकाऊ तथा आवश्यकतानुसार अधिक-से-अधिक उपयोगी होना चाहिए।
प्रश्न 5
लकड़ी के फर्नीचर की देख-रेख कैसे करेंगी?
उतर:
उम्र लकड़ी के फर्नीचर की देख-रेख के लिए उन पर समय-समय पर पॉलिश तथा प्रतिदिन सफाई करनी अति आवश्यक है।
प्रश्न 6
संयुक्त स्नानघर से आप क्या समझती हैं?
उत्तर:
संयुक्त स्नानघर में स्नानघर व शौचालय साथ-साथ होते हैं। यह प्राय: कमरों से संलग्न होते हैं।
प्रश्न 7
फूलदान में फूल जल्दी न सूखे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगी?
उतर:
उम्र फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए फूलदान का पानी प्रतिदिन (UPBoardSolutions.com) बदल दिया जाना चाहिए तथा इस पानी में थोड़ा-सा नमक मिला देना चाहिए।
![]()
प्रश्न 8
‘इकेबाना’ पुष्प-सज्जा से आप क्या समझती हैं?
उतर:
उक्ट इस आधुनिक पुष्प-सज्जा में फूल-पत्तियों के साथ छोटी-छोटी सूखी टहनियों, घास-फूस एवं छोटी-छोटी कलात्मक वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है। यह मूल रूप से पुष्प-सज्जा की एक जापानी शैली है।।
प्रश्न 9
“घर की अच्छी सजावट अर्थव्यवस्था से नहीं, परन्तु गृहिणी की अभिरुचि से होती है।” स्पष्ट कीजिए। या । अधिक धन के खर्च के बिना घर की सजावट कैसे कर सकते हैं ? [2009, 18]
उत्तर:
आदर्श गृहिणी मितव्ययिता के साथ अपनी कलात्मक अभिरुचि के आधार पर घर की अच्छी सजावट कर सकती है।
प्रश्न 10
घर की उपयुक्त सजावट गृहिणी के किन गुणों की परिचायक है?
उत्तर:
घर की उपयुक्त सजावट गृहिणी की सूझ-बूझ, सुरुचि एवं सुघढ़ता की परिचायक होती है।
प्रश्न 11
घर की सजावट के लिए अपने आप से तैयार की जाने वाली दो सजावट की वस्तुओं के नाम लिखिए। [2010]
उत्तर:
स्वयं तैयार की जा सकने वाली सजावट की वस्तुएँ हैं-लैम्पशेड तथा फोटोफ्रेम।
![]()
प्रश्न 12
सजावट की कला के प्रमुख सिद्धान्त कौन-कौन से हैं? [2011, 12, 16]
उत्तर:
सजावट की कला के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं
- अनुरूपता,
- सन्तुलन तथा
- समानुपात।।
प्रश्न 13
घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्त्व है? [2011, 12, 13, 14]
या
घर में पुष्प सज्जा के दो महत्त्व लिखिए। [2012, 13]
उत्तर:
अपने आकर्षक रंगों एवं सुगन्ध के कारण फूल घर की सजावट में अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। इनका गुच्छा आदि बनाकर फूलदानों व अन्य पात्रों में घर के विभिन्न भागों में सजाया जाता है।
प्रश्न 14
गृह-सज्जा के लिए अपनाई जाने वाली पुष्प-व्यवस्था की जापानी शैली को क्या कहते हैं?
उत्तर:
इकेबाना।
प्रश्न 15
कमरे के लिए परदे का चुनाव कैसे करेंगी? [2012, 13]
उत्तर:
कमरे की दीवारों का रंग एवं कालीन के रंग एवं डिजाइन को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप ही परदों के रंग व डिजाइन का चुनाव करना चाहिए।
प्रश्न 16
कमरे में परदे लगाने के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। [2010, 11, 12, 13]
उत्तर:
- तेज रोशनी, लू एवं ठण्डी हवा से बचाव करना तथा
- कमरे के अन्दर एकान्तता प्रदान करना और कमरे (UPBoardSolutions.com) की सज्जा में वृद्धि करना।
![]()
प्रश्न 17
फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं ? [2014, 17]
उत्तर:
फर्नीचर अनेक प्रकार के होते हैं; जैसे-लकड़ी का फर्नीचर, पाइप का फर्नीचर, माइका लगा फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, फोम का फर्नीचर तथा रेक्सीन लगा फर्नीचर। अब फाइबर-ग्लास का भी फर्नीचर बनने लगा है।
प्रश्न 18
गृह-व्यवस्था किसे कहते हैं ? [2017]
उत्तर:
गृह के सभी कार्य पूर्ण रूप से होना, आय और व्यय में ताल-मेल बनाए रखना तथा घर की सफाई का भी ध्यान रखना गृह-व्यवस्था कहलाती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न-निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्पों का चुनाव कीजिए
प्रश्न 1.
सजावट का क्या अर्थ है? । [2016]
(क) परदे लगाना
(ख) चित्रों से घर सजाना
(ग) फूलों से घर सजाना
(घ) घर सुव्यवस्थित रखना
प्रश्न 2.
सजावट से पूर्व आवश्यक है- [2011, 16]
(क) चित्र एकत्र करना
(ख) कालीन खरीदना
(ग) फूलों का चुनाव करना
(घ) कमरे की सफाई करना
प्रश्न 3.
घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है {3}
(क) सफाई
(ख) मूल्यवान कालीन
(ग) दुर्लभ कलाकृतियाँ
(घ) विदेशी फर्नीचर
प्रश्न 4.
गृह-सज्जा का आवश्यक तत्त्व है [2008, 15, 17]
(क) उपयोगिता
(ख) सुन्दरता
(ग) अभिव्यक्ति
(घ) ये सभी
प्रश्न 5.
फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? [2009, 12]
(क) सोडा
(ख) नमक
(ग) साबुन
(घ) दूध
प्रश्न 6.
बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए|
(क) फूलों के ।
(ख) बालोपयोगी
(ग) कलात्मक
(घ) श्रृंगारिक
प्रश्न 7.
घरेलू फर्नीचर का मुख्यतम गुण है उसका
(क) नक्काशीदार होना
(ख) अधिक-से-अधिक सजावटी होना
(ग) उपयोगी होना
(घ) सस्ता होना
![]()
प्रश्न 8.
सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है?
(क) रसोईघर की
(ख) भोजन के कमरे की
(ग) ड्राइंग-रूम की
(घ) शयन-कक्ष की
प्रश्न 9.
घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? [2015]
(क) ईंट
(ख) बालू
(ग) सीमेन्ट
(घ) फूलदान
प्रश्न 10.
घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है? [2017]
(क) फूलदान
(ख) चित्र
(ग) हथौड़ा
(घ) कालीन
उतर:
- (घ) घर सुव्यवस्थित रखना,
- (घ) कमरे की सफाई करना,
- (क) सफाई,
- (घ) ये सभी,
- (ख) नमक,
- (ख) बालोपयोगी,
- (ग) उपयोगी होना,
- (ग) ड्राइंग-रूम की,
- (घ) फूलदान,
- (ग) हथौड़ा।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Home Science गृह विज्ञान Chapter 3 घर की सफाई help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Home Science गृह विज्ञान Chapter 3 घर की सफाई drop a comment below and we will get back to you at the earliest.