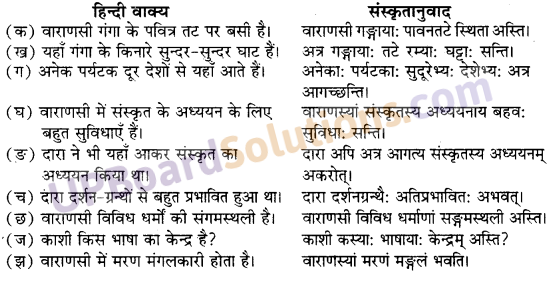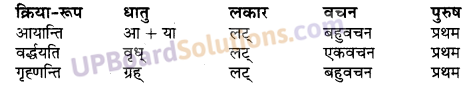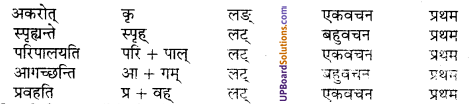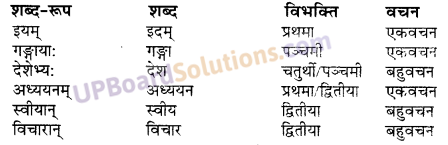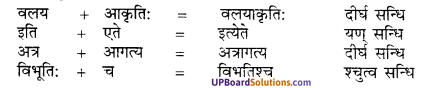UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 कर्मवीर भरत (खण्डकाव्य)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 कर्मवीर भरत (खण्डकाव्य).
प्रश्न 1
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। [2010, 12, 14, 17]
या
‘कर्मवीर भरत’ के कथानक का सारांश अथवा कथासार लिखिए। [2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य में वर्णित प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
या
‘कर्मवीर भरत’ की किसी प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। [2017]
उत्तर
कर्मवीर भरत खण्डकाव्य की कथावस्तु अत्यन्त रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक चिर-परिचित रामकाव्य का एक लघु, किन्तु महत्त्वपूर्ण अंश है। इसमें भरत को मानव-सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग-युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से सँवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हैं
(1) आगमन-इसमें अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुँचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृत्तान्त वर्णित है और अयोध्या में व्याप्त शोकपूर्ण वातावरण के साथ-साथ तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है।
(2) राजभवन–इस सर्ग में भरत-कैकेयी मिलन के साथ-साथ (UPBoardSolutions.com) राम-वन-गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन-सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था किसी लोभ या कठोरता के कारण नहीं। सर्ग के अन्त में अपनी नीति-कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत, शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं।
(3) कौशल्या-सुमित्रा मिलन-इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएँ उनकी आत्म-ग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन-पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अन्त में सुमित्रा भरत से कहती है कि “तुम अपने मन के क्षोभ का त्याग कर दो और हम सबके पथ-प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।

(4) आदर्श वरण—इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के सम्बन्ध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं। ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह-संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमन्त भरत के राजतिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अयोध्या के राजसिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते
(5) वन-गमन–इस सर्ग में भरत के वन-प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषादराज की रामभक्ति एवं सेवा-भावना का भी सुन्दर वर्णन हुआ है। निषादराज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। रार्म’ के चित्रकूट (UPBoardSolutions.com) में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं।
(6) राम-भरत-मिलन–इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं, तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं, स्वयं नन्दिग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं।
प्रश्न 2
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकोष के प्रथम (आगमन) सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए।।[2010]
या
कर्मवीर भरत के आधार पर संक्षेप में बताइए कि भरत के अयोध्या लौटने पर उन्हें अयोध्या | किस रूप में दिखाई दी ? [2009]
उत्तर
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है। चौदह वर्ष के लिए राम के वन-गमन और दशरथ की मृत्यु के पश्चात् दूत द्वारा भरत को ननिहाल से बुलाये जाने की घटना से कथा का आरम्भ होता है।
दूतों का ननिहाल पहुँचना एवं भरत की शंका–गुरु वशिष्ठ के आदेश से अयोध्या के दूत कैकेयराज के यहाँ पहुँचकर, भरत को गुरु के द्वारा शीघ्र बुलाये जाने का सन्देश देते हैं। दूतों के मुख से शीघ्र बुलाये जाने का गुरु-आदेश सुनकर भरत का मन व्याकुल हो जाता है। उनके मन में बार-बार यह शंका उठती है कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो राम-लक्ष्मण के रहते मुझे बुलाया जा रहा है ? भरत दूतों से पुरवासियों, गुरु वशिष्ठ, पिता (UPBoardSolutions.com) दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, भाई राम और लक्ष्मण की कुशलक्षेम पूछते हैं। दूतों ने दशरथ-मृत्यु और राम के वन-गमन की बात को छिपाकर सभी का कुशल समाचार सुनाया।
भरत का प्रस्थान–शंकालु और चिन्तित भरत ने अपने मामा से गुरु का आदेश बताकर उनकी अनुमति से अयोध्या-प्रस्थान की तैयारी की। वे पर्वत, नदी और वनों को पार करते हुए सात दिन में अयोध्या के सालवन में पहुँचे। मार्ग में भरत को प्रकृति भी उदास दिखाई देती है। उन्हें उषाकाल में भी सूनापन, हरियाली में भी सूखापन तथा आलोक में भी तम दिखाई दे रहा था।
अयोध्या-प्रवेश नगर में प्रवेश कर अयोध्या के सूनेपन को देखकर भरत का मन व्याकुल हो गया। उन्हें भवन वन्दनवारों से रहित, गलियाँ सूनी और घरों के आँगन बिना बुहारे हुए दिखाई दिये। उन्होंने गायों को व्याकुलता से सँभाते और वायु को साँय-साँय करते हुए कुछ अजीब-सा अनुभव किया।
अयोध्या का सूनापन-भरत ने अयोध्या को वैभवहीन, शंख-ध्वनिविहीन, यज्ञ को धूम से रहित देखा। अयोध्या पर गिद्धों को मँडराते एवं मार्गों को आवागमन से रहित, बाजारों को अस्त-व्यस्त, देवमन्दिरों के द्वार बन्द और भवनों को पताकारहित देखकर भरत के मन में अत्यधिक चिन्ता हुई। उनके बायें अंग फड़कने लगे और हृदय में शंका छा गयी। उदास पुरवासी मौन संकेतों से बातें कर रहे थे। उन्होंने राजद्वार पर द्वारपालों को मौन ठगे-से खड़ा देखा।

राजगृह की दशा-राजगृह में बन्दी-सूत यशोगान नहीं कर रहे थे। उन्हें कोई मन्त्री नहीं दिखाई दिया। मंगल गीत न गाये जाने से राजभवन सोया-सोया-सा लग रहा था। उन्हें पिता दशरथ का कक्ष भी सूना दिखाई दिया। अब उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका (UPBoardSolutions.com) सताने लगी। चिन्तामग्न भरत, कैकेयी के कक्ष की ओर चले गये।
प्रश्न 3
‘कर्मवीर भरत’ के द्वितीय सर्ग अथवा राजभवन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। [2010, 11, 12, 13]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के दूसरे सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने के कौन-से कारण प्रस्तुत किये गये हैं ? उन्हें स्पष्ट कीजिए। [2010, 12]
या
‘कर्मवीर भरत खण्डकाव्य के द्वितीय सर्ग ‘राजभवन में वर्णित घटनाओं पर प्रकाश डालिए। [2018]
उत्तर
कर्मवीर भरत के राजभवन’ नामक द्वितीय सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने का कारण एवं भरत की आत्मग्लानि व्यक्त हुई है। कैकेयी ने भरत को देखकर प्रेम से गले लगाया और अपने मातापिता का कुशलक्षेम पूछा। भरत उनके पितृ-गृह का कुशलक्षेम बताकर उनसे अयोध्यापुरी की विकलती को कारण पूछते हैं। |
दशरथ की मृत्यु का कारण-कैकेयी ने भरत को बताया कि राम अयोध्या में रहकर युगों से अभिशप्त व अभावों से पूर्ण वनवासियों की रक्षा न कर सकेंगे; अत: तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए अयोध्या को राज्य माँगकर और राम को वन में भेजकर मैंने अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुमको अयोध्या का राज्य देने की मेरी पहली बात तो मान ली, परन्तु राम-वन-गमन की दूसरी माँग सुनकर प्राण-त्याग दिये।
राम को वन भेजने के कारण-कैकेयी कहती है कि यद्यपि लोग मुझे नीच, झूमर और स्वार्थी कहकर कलंकित करेंगे, परन्तु मैंने जन-जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही राम को धम भेजने का वर माँगा था। राम में पौरुष और प्रतिभा है तथा मानवमात्र का (UPBoardSolutions.com) कल्याण करने की उदात्त भावना है। उन्हें सिंहासन का मोह नहीं है, यही सोचकर मैंने असभ्य, अशिक्षित एवं अभावग्रस्त वनवासियों के कल्याण हेतु राम को चौदह वर्ष के लिए वन भेजने का वर माँगा था। यह सुनकर तुम्हारे सत्यनिष्ठ पिता ने अपने प्राण त्याग दिये। जब मैंने पाषाण-हृदय बनकर, ममता को त्यागकर राम को उनके वनवास की बात बतायी तो वे प्रसन्न होकर, वल्कल पहनकर सीता और लक्ष्मण के साथ तत्काल वन को चल दिये।

भरतं को शोक-अपनी माता के मुख से यह करुण कहानी सुनकर भरत स्तब्ध रह गये और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे ‘हाय पिता! हाय राम!’ कहकर भूमि पर गिर पड़े तथा खिन्न होकर अपने आभूषण उतार फेंके। अपने हाथों से घर में आग लगाने वाली अपनी माता की नीति उन्हें अच्छी न लगी। तीनों लोकों में उन्हें ऐसी रानी नहीं दिखाई पड़ी, जिसने एक साथ अपने पति को मृत्युलोक और पुत्र को वन भेज दिया हो। भरत ने कैकेयी से कहा-“तुम्हारे द्वारा मेरे लिए राज्य माँगने के पीछे सभी लोग उसे मेरी ही इच्छा बताएँगे। हमारे वंश में बड़े पुत्र का राजतिलक होने की परम्परा है। यदि तुम चारों पुत्रों को वन में भेज देतीं तो तुम्हारा त्याग अमर हो जाता। तुम भरत को राज्य दिलाकर और राम को वन में भिजवाकर अपने कार्य-कौशल व बुद्धिमत्ता की दुहाई दे रही हो।”
राम में अलौकिक शक्ति-अन्त में कैकेयी ने समझाया कि तुम राम की असीम शक्ति पर विचार न करके मात्र वन की भयंकरता से डर रहे हो। उन्होंने वीर क्षत्राणी का पय-पान किया है; विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का (UPBoardSolutions.com) वध किया है तथा जनकपुर में रावण के गर्व को चूर कर और सीता का वरण करके अपनी शक्ति की महिमा स्थापित की है। अत: तुम शोक न करके जनहित के कार्य में लग जाओ।
अपनी नीति-कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जान मन में शोक का भार लिये भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं।
प्रश्न 4
‘कर्मवीर भरत’ के ‘कौशल्या-सुमित्रा-मिलन’ शीर्षक तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। [2011, 12, 13, 15]
या
‘कर्मवीर भरत’ के आधार पर भरत के कौशल्या तथा सुमित्रा से हुए वार्तालाप का वर्णन संक्षेप में कीजिए। [2009]
उत्तर
भरत और कौशल्या-मिलन–कौशल्या के भवन में जाकर दोनों भाइयों ने माता के चरणों की वन्दना की और उनसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय माता कौशल्या के केश बिखरे हुए, वस्त्र मलिन, तन आभूषणरहित और आँखों में आँसू भरे हुए थे। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले लगाकर बिलख-बिलखकर रोते हुए, मन के विषाद को कम किया।
भरत ने माता कौशल्या से कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। यदि पिता जीवित रहते तो मेरे सौ-सौ अपराध क्षमा कर देते। मैं अपनी माता की नीति नहीं समझ पाया। अयोध्या का राज्य मेरे । लिए शूल बना हुआ है। यह कभी नहीं हो सकता कि राम वन में रहें और भरत राज्य-सुख भोगता रहे। यह कहकर भरत ने माँ कौशल्या के चरण पकड़ लिये।।
माता कौशल्या ने भरत को गले लगाकर कहा कि इसमें न तो तुम्हारा (UPBoardSolutions.com) कोई दोष है और न ही कैकेयी का। कैकेयी तो हमेशा राम का हित चाहती थी। राम भी उसका ही सर्वाधिक आदर करते थे। उसने भी अपना हृदय कठोर बनाकर ही जीवन-दीक्षा के लिए राम को वन भेजा है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का हीन भाव न लाओ।,

कौशल्या ने पुन: कहा कि यह तो सभी जानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं है। तुम अपने मन की शंका और ग्लानि को दूर कर आत्मविश्वासपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तक सरयू की धारा है, तब तक तुम्हारा सुयश रहेगा। इस प्रकार माता कौशल्या ने अपने स्नेह-सिक्त वचनों से भरत का उत्साह बढ़ाया तथा उन्हें समझाया कि अन्त:करण को शुद्ध रखने वाले साहसी पुरुष कभी परनिन्दा पर ध्यान नहीं देते। जो निन्दा व अपयश के भयजाल में फंसे रहते हैं वे जीवन में कभी महान् कार्य नहीं कर सकते।
भरत और सुमित्रा-मिलन–राजभवन में भरत के आने का समाचार सुनकर सुमित्रा उनसे मिलने दौड़ीं और भाव-विह्वल होकर उन्होंने पुत्रों को गले से लगाया। भरत ने सुमित्रा से कहा-“हे माँ! तुमने श्रीराम को वन जाने से क्यों नहीं रोका? मेरी माता ने मुझे राज्य का लोभी जानकर मेरे सिर पर राजमुकुट रख दिया और राम के सिर पर जटा-मुकुट। यही शूल हृदय में चुभ रहा है। काश! वह मुझे वन भेज देतीं तो आज राम अवध का शासन करते।’
भरत की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा- “बेटा, तुम्हारी शिक्षा अयोध्या तक सीमित रही है और राम ने पहले भी विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों का वध किया है। वे वन के कष्टों से भली-भाँति परिचित हैं। मुझे तुम्हारा मलिन मुख देखकर रोना आता है। मैंने वैधव्य तो सहन कर लिया, परन्तु तुम्हें दुःखी देखकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नववधू उर्मिला, जिसने हँसते-हँसते पति लक्ष्मण को वन भेजा है, वह भी अपने अन्तर के दु:ख को प्रकट (UPBoardSolutions.com) नहीं होने देती, लेकिन तुम्हें विकल देखकर वह भी धैर्य धारण नहीं कर सकेगी। उधर वधू माण्डवी भी तुम्हें दु:खी देखकर अपने आँसू नहीं रोक पाएगी। अतः तुम अपने मन का क्षोभ त्यागकर हमारे पथ-प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य को निभाओ।” इस प्रकार सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को प्रेम से गले लगाकर गुरु के पास भेज दिया।
प्रश्न 5
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के चतुर्थ सर्ग ‘आदर्श वरण’ का सारांश लिखिए। [2011, 12]
या
“चतुर्थ सर्ग ‘आदर्श वरण’ में सच्चे अर्थों में भरत की कर्मवीरता व्यक्त हुई है। उदाहरण सहित इस कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए। [2010]
या
‘कर्मवीर भरत’ के चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। [2017]
उत्तर
गुरु का समझाना–भरत और शत्रुघ्न गुरु के पास पहुँचे और उनके चरणों में नमन कर संकोच के कारण कुछ भी कह न सके। गुरु ने आशीर्वाद देकर भरत को उनके वर्तमान कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दशरथ सत्य का पालन करने के कारण मरकर भी अमर हो गये; अतः अब तुम चिन्ता को छोड़कर पिता के शरीर का विधिवत् संस्कार करो। पिता के निर्जीव शरीर को देखकर भरत मूर्च्छित हो गये। चेतना लौटने पर वशिष्ठ ने (UPBoardSolutions.com) भरत का हाथ पकड़कर उन्हें संसार की नश्वरता समझायी और कहा कि “नाश और विकास, सुख और दुःख, मृत्यु और जीवन साथ-साथ चलते रहते हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं। केवल ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है।”

दशरथ का अन्तिम संस्कार-दशरथ के मृत शरीर को एक पालकी में रखकर सरयू-तट पर लाया गया। पुरवासी विकल होकर पीछे-पीछे चल रहे थे। भरत ने पिता के भौतिक शरीर का दाह-संस्कार किया और श्रद्धापूर्वक स्वर्ण-मणियों का दान दिया।
भरत के अभिषेक का प्रस्ताव तथा भरत का राम को लौटा लाने का संकल्प-स्नानादि से शुद्ध होकर गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा बुलायी गयी। सुमन्त ने भरत के राज्याभिषेक को शास्त्रसम्मत, लोकसम्मत और पिता की आज्ञा बताते हुए उनके राजतिलक का प्रस्ताव रखा। सुमन्त की बात सुनकर भरत ने विनय सहित कहा कि रघुकुल की युगों से रीति रही है कि बड़ा पुत्र ही शासन का अधिकारी होता है। अतः परम्परा-निर्वाह के लिए त्यागपूर्वक सिद्धान्तों की रक्षा करना ही उचित है। राम संन्यासी होकर वन में चले गये, जिसके कारण पिता स्वर्ग सिधार गये। फिर वही राज्य मैं ग्रहण करू, यह कैसे सम्भव है? मैं वन में । जाकर, राम के चरण पकड़कर उनको लौटाकर लाऊँगा और माँ के द्वारा लगाये गये कलंक को मिटाऊँगा
वन में राम रहें, मैं बैर्दै सिंहासन पर,
शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दें गुरुवर ।
वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊँ,
जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊँ ॥
भरत के वचन सुनकर दु:ख के समुद्र में डूबते हुए सबको मानो जीने का सहारा मिल गया। भरत के दृढ़ संकल्प को सुनकर शत्रुघ्न, कैकेयी सहित सभी माताओं, पुरवासियों और वशिष्ठ ने राम को अयोध्या लौटाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर तक तो भरत पैदल (UPBoardSolutions.com) ही चले किन्तु माता कौशल्या के कहने पर रथ पर बैठ गये। दिन-भर चलने के पश्चात् सभी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और प्रात: गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर नदी को पार करके आगे बढ़े।

प्रश्न 6
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के ‘वन-गमन’ शीर्षक पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। [2016, 18]
उत्तर
निषादराज की शंका-श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर भरत के पहुँचने का समाचार पाकर और रथ पर इक्ष्वाकु वंश की पताका लहराती देखकर निषादराज के मन में शंका उत्पन्न हो गयी कि कहीं राम को वन में अकेले जानकर राजमद में चूर भरत सेना सहित वन में विघ्न डालने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसने सभी निषादों के साथ मिलकर निश्चय किया कि हम किसी को भी गंगा पार न जाने देंगे। उसी समय एक वृद्ध निषाद ने कहा कि पहले उनके आने का रहस्य जान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या भी उनके साथ हैं।
भरत का सम्मान–वृद्ध की बात सुनकर बिना विचारे अपने वीरभाव दर्शाने पर लज्जित निषादराज ” ने भरत के सत्कार हेतु कन्द-मूल-फल मँगाये। गुरु वशिष्ठ की बातों से तो निषादराज गद्गद हो गये तथा भरत के समीप पहुँचने व उनके अपार स्नेह से अत्यधिक पुलकित हो गये। (UPBoardSolutions.com) उनका यथोचित सत्कार करके नावों द्वारा सबको पार ले गये। यहाँ भरत भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग पहुँचे। वहाँ से चित्रकूट में राम के निवास का समाचार प्राप्त कर तथा चित्रकूट को समीप जानकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही आगे की ओर चल दिये।
प्रश्न 7
‘कर्मवीर भरत’ के षष्ठ सर्ग ‘राम-भरत-मिलन’ का सारांश लिखिए। [2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के षष्ठ सर्ग (अन्तिम सर्ग) की कथा लिखिए।
उत्तर
सेना सहित भरत को सहसा वन में आते देखकर एक भील ने रामचन्द्र जी को भरत-आगमन का समाचार सुनाया। लक्ष्मण को मन कुछ शंकित हुआ, परन्तु भरत का नाम सुनकर पुलकित होकर राम चरण-पादुका के बिना ही कुटी के बाहर आ गये। उन्होंने धूल-धूसरित (UPBoardSolutions.com) भरत को अपने चरणों में नत देखा तो भरत को स्नेह सहित उठाकर गले से लगा लिया। शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किये। इसके बाद दोनों भाइयों ने सीता के चरणों में शीश झुकाकर ‘सदा सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त किया।
गुरु का आगमन सुनकर राम उनके रथ के पास गये और आदर सहित उन्हें आश्रम में ले आये। माताओं के चरण छूकर और सुमन्त से भेंट करके राम अति हर्षित हुए। गुरु वशिष्ठ से पिता की मृत्यु की बात सुनकर व्याकुल होकर ‘हाय पिता’ कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गुरु के समझाने पर तर्पणादि कार्य करके निवृत्त हुए।

चित्रकूट में राम के प्रेम में विभोर हुए सभी के कई दिन बीत गये। चित्रकूट के वन-उपवनों की प्राकृतिक सुषमा ने उनका मन मोह लिया था। भरत संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे थे। तब वशिष्ठ ने कहा कि हमको यहाँ आये बहुत दिन बीत गये हैं, अब हमें लौटना चाहिए। तब अवसर पाकर भरत ने कहा कि मैं राम को छोड़कर अयोध्या नहीं जाऊँगा। मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वन में निवास करूंगा। हम सबकी विनती स्वीकार कर राम अयोध्या जाएँ, सिंहासन सूना पड़ा है। तत्पश्चात् कैकेयी ने राम से कहा-“पुत्र! मैं इस दु:खमय नाटक की सूत्रधारिणी हूँ। तुम भरत के कहे अनुसार राज्य प्राप्त करके मेरे ऊपर लगे कलंक को (UPBoardSolutions.com) मिटाओ।” गुरु ने भी कैकेयी का समर्थन किया। कैकेयी के वचन सुनकरे राम ने कहा-“माता! इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। काल की गति ही वक्र है। मैं विवश हूँ, लौटकर नहीं जा सकता। भरत को राज्य का मोह नहीं है, फिर भी मैं अयोध्या जाकर राज्य नहीं कर सकता। भरत धर्मनिष्ठ होकर भी प्रेम-सिन्धु में डूब रहा है। यदि वह कहे तो मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर अयश के सागर में डूब सकता हूँ, परन्तु कुल के आदर्शों को तो निबाहना ही चाहिए।’ |
भरत ने कहा–“हे प्रभु! मैं नन्दिग्राम में कुटी बनाकर सिंहासन पर आपकी चरण-पादुकाएँ रखकर चौदह वर्ष तक वनवासी की तरह निवास करूंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर जनसेवा करता रहूंगा। मैं आपकी पादुकाएँ लिये बिना नहीं जा सकता। आप मुझे चौदह वर्ष की अवधि बीतने पर लौट आने का आश्वासन दीजिए।’ यह कहकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े।
‘राम ने अपनी चरण-पादुकाएँ दे दीं और सबको प्रेम सहित विदा किया। भरत ने अयोध्या न जाकर नन्दिग्राम में कुटी बनायी और सिंहासन पर राम की चरण-पादुकाएँ रख दीं। शत्रुघ्न भरत की आज्ञा से राज्य का कार्य चलाने लगे। इस प्रकार भरत ने अपने चरित्र का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया।
प्रश्न 8
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के आधार पर उसके नायक (प्रधान पात्र) भरत का चरित्र-चित्रण कीजिए। [2009, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य का नायक कौन है ? उसका चरित्र-चित्रण कीजिए। [2009, 14]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताएँ लिखिए। [2009, 11, 13, 16, 18]
या
‘कर्मवीर भरत’ के आधार पर भरत के चरित्र की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
या
‘कर्मवीर भरत’ में भरत को कर्मवीर क्यों कहा गया है ? स्पष्ट कीजिए। [2009, 10, 11, 12, 14]
या
“भरत तप, त्याग और शील पर दृढ़ रहने वाला उदात्त चरित्र है।” ‘कर्मवीर भरत खण्डकाव्य के आधार पर इस कथन को प्रमाणित कीजिए। [2009]
या
भरत को कर्मवीर की उपाधि क्यों दी गयी ? स्पष्ट कीजिए। [2015]
उत्तर
श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र ‘निशंक’ द्वारा रचित ‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य का नायक (UPBoardSolutions.com) भरत है। काव्य में आदि से अन्त तक उनके कार्य एवं चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
(1) आज्ञाकारी-भरत अपने मामा के यहाँ गये हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरन्त अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं।

(2) राज्य के लोभ से रहित-भरत को राज्य-वैभव को लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वे अत्यन्त दु:खी होकर माता से कहते हैं-
भरत करेगा राज्य, राम को भेज विजन में ।
जानें क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में।
वे जीवन के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं। कौशल्या भी भरत को सर्वथा राज्य-लोभ से रहित मानती हैं। यद्यपि सभी माताएँ, गुरु वशिष्ठ, सुमन्त आदि सभी एक मत से भरत से राजा बनने का आग्रह करते हैं फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम को वन से लौटा लाने और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव करते हैं। वन से लौटकर नन्दिग्राम में कुटी बनाकर; वनवासी का जीवन व्यतीत करना राज्य के प्रति उनकी अनासक्ति का परिचायक है।
(3) मर्यादा एवं कर्त्तव्य के पालक–भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा (UPBoardSolutions.com) और कर्त्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के समस्त सुखों को भी न्योछावर कर देते हैं। वे कहते हैं-
किन्तु ज्येष्ठ को राजतिलक की परम्परा है।।
राजा दुःख से नहीं, अनय से सदा डरा है।।
भरत चौदह वर्ष तक नन्दिग्राम में वनवासी की तरह रहकर सिंहासन पर राम की पादुकाएँ रखकर सेवक बनकर राम के राज्य की देखभाल स्वीकार करते हैं। वे कुल की मर्यादा और नीति की रक्षा के लिए बड़े-से-बड़ा त्यागकर कर्तव्य का पालन करने में गौरव मानते हैं।
(4) भ्रातृ-प्रेमी-भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रातृ-प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ है। सबके द्वारा एक मत से उनके लिए राजतिलक का प्रस्ताव करने पर भी वे कहते हैं-

वन में राम रहें, मैं बैटू सिंहासन पर,
शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दें गुरुवर
वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊँ,
जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊँ ॥
वे राम को लौटाने का दृढ़ संकल्प कर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काव्य में आदि से अन्त तक वे राम-वन-गमन की चिन्ता से व्यथित रहते हैं।
(5) सच्चे योगी-भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं तथा राजसुख को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगो का जीवन बिताते हैं, वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। वे नन्दिग्राम में कुटी बनाकर कुश-आसन पर बैठकर राज्य-कार्य का संचालन करते हैं।
इस प्रकार भरते आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादापालक, राज्य-लोभ से दूर, भ्रातृ-प्रेमी और (UPBoardSolutions.com) सच्चे कर्मयोगी हैं। साथ ही उनमें पितृ-भक्ति, गुरु-निष्ठा, निश्छलता, स्पष्टवादिता, विनम्रता आदि गुण निहित हैं। वे त्याग की साक्षात् मूर्ति, शील और संयम के साक्षात् अवतार तथा आदर्श महापुरुष हैं। उनका चरित्र महान् और अनुकरणीय है।
प्रश्न 9
‘कर्मवीर भरत’ के आधार पर कैकेयी का चरित्र-चित्रण कीजिए। [2009, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18]
या
” ‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य में कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वल बनाकर भारतीय नारी को गौरव प्रदान किया गया है।” खण्डकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। [2010, 11]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। [2010]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के आधार पर किसी प्रमुख नारी-पात्र का चरित्र-चित्रण कीजिए।
उत्तर
‘कर्मवीर भरत’ के स्त्री पात्रों में कैकेयी का चरित्र सर्वोपरि है। उसमें साहस, दृढ़ता, राजनीतिक कुशलता, विवेकशीलता, जनहित भावना, पुत्र-प्रेम आदि आदर्श भारतीय नारी के गुण विद्यमान हैं। इस खण्डकाव्य में उसके चरित्र को उज्ज्वल दर्शाकर भारतीय नारी को गौरव प्रदान किया गया है। उसके चरित्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं.
(1) युद्ध-निपुण वीरांगना–कैकेयी का चरित्र एक वीरांगना का चरित्र है। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर जनहित के लिए अपने पुत्र को चौदह वर्ष के लिए वन में भेज देती है। उसने नारी होकर भी अबला बनना नहीं सीखा है। युद्ध-भूमि में भी वह अपने पति के साथ गयी थी और संकट में उनके प्राणों की रक्षा की थी। उसे जो कार्य उचित जान पड़ता है, लोकमत के विरुद्ध होने पर भी वह उसे करके ही छोड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियों से उसका वीरत्व प्रकट होता है—

असि अर्पण कर मैंने रण कंकण बाँधा है,
रणचण्डी का व्रत मैंने रण में साधा है ।
मेरे बेटों ने पय पिया सिंहनी का है,
उनका पौरुष देख इन्द्र मन में डरता है ।।
(2) आदर्श माता–कैकेयी स्वाभिमानी होने के साथ-साथ आदर्श माता भी है। वह अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती, अपितु उनके गौरव को भी बढ़ाना चाहती है। वह प्रत्येक पुत्र के जीवन का विकास उसकी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहती है, जिससे वे समाज, राष्ट्र और मानवता की अधिकाधिक सेवा कर सकें। वह राम और भरत में भेद नहीं मानती-
राम-भरत में भेद ? हाय कैसी दुर्बलता,
आगे चलते राम, भरत तो पीछे चलता।
वह राम को इसलिए वन में भेजती है, जिससे वह वन में जाकर दुष्टों और आततायियों का विनाश कर मानवता का कल्याण कर सके। उसने राम को वन में भेजकर मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मातृत्व धर्म की दृढ़ता से रक्षा की है।
(3) राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली आदर्श नारी-कैकेयी के (UPBoardSolutions.com) चरित्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता उसका राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण है। उसकी विचारधारा केवल अपने पुत्रों और परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह सम्पूर्ण राष्ट्र और मानवता का भी कल्याण सोचती है। उसे केवल अयोध्यावासियों के ही कल्याण का ध्यान नहीं है, अपितु पिछड़े हुए अशिक्षित वनवासियों के उत्थान का भी वह ध्यान रखती है। उसका मानवीय दृष्टिकोण अत्यधिक उदार है-
जिन्हें नीच पामर कहकर हम दूर भगाते ।
वे भी तो अपने हैं मानवता के नाते ॥
उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं है।
गले लगाना क्या मानव का कर्म नहीं है।
(4) राजनीति में कुशल-कैकेयी नारी होकर भी राजनीति में पूर्ण कुशल है। वह राजनीति के दाँव-पेच समझती है और समय के अनुसार उनका प्रयोग करना भी जानती है। राम को वन भेजने में भी उसकी राजनीतिक सूझ-बूझ का प्रमाण मिलता है। वनवासियों को अनुशासन सिखाना भी एक राजनीतिक दायित्व है।

(5) अपराध स्वीकार करने वाली-खण्डकाव्य के कथानक के अनुसार कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था और न कोई बुरा भाव ही था। परन्तु जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तथा परिणाम बुरे निकलने लगते हैं तो कैकेयी अपने आपको अपराधिनी स्वीकार कर लेती है तथा । स्वयं ही अपने विषय में कह उठती है
इस दुःखान्त नाटक की मैं हूँ सूत्रधारिणी।
हरे-भरे रघुकुल में प्रलय-विनाशकारिणी ॥
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत खण्डकाव्य में कैकेयी आदर्श माता, वीर (UPBoardSolutions.com) स्त्री तथा समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श नारी है। उसमें साहस, दृढ़ता, सूझ-बूझ और उदारता है। निशंक जी ने कैकेयी के युग-युग से अभिशप्त चरित्र को आधुनिक परिवेश में सँवारने का सफल प्रयत्न किया है।
प्रश्न 10
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के नायक (प्रमुख पात्र) के अतिरिक्त किस पात्र के चारित्रिक गुणों से आप प्रभावित हैं ? उन गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। [2010, 14]
या
‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के किसी प्रमुख पात्र का चरित्रांकन कीजिए। [2013]
उत्तर
कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका चरित्र-चित्रण अन्तिम सर्ग में (UPBoardSolutions.com) हुआ है, किन्तु उससे पूर्व कैकेयी, सुमित्रों आदि के कथन भी उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं।

(1) संकल्पवान् राम सिद्धान्तप्रिय हैं। वे एक बार जो संकल्प कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही मानते हैं। इसीलिए वे भरत और परिजनों के अत्यधिक आग्रह करने पर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते और अयोध्या वापस नहीं लौटते। वे स्पष्ट रूप से कह देते हैं
क्षमा करें सब लोग, विवशता मेरे मन की,
अपनायी है कठिन राह मैंने जीवन की ।
इतना होने पर भी अब मैं पुर को जाऊँ ?
राज्य करू या पुत्रधर्म आदर्श मिटाऊँ ?
(2) संवेदनशील सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ होते हुए भी वे भरत के शील और भक्ति के सम्मुख भाव-विह्वल हो जाते हैं। उनके मन में भरत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है। वे भरत के आग्रह से प्रसन्न होकर कह उठते हैं-
भाई जो भी कहो वही मैं आज करूंगा।
तुम कह दो तो अयश सिन्धु में कूद पड़ेंगा ॥
(3) मर्यादा पुरुषोत्तम-राम ने भरत की बात मानकर उन्हें अपनी खड़ाऊँ दे दी और सबको (UPBoardSolutions.com) ससम्मान विदा किया। उन्होंने कहीं भी मर्यादा की सीमा-रेखा नहीं लाँघी। वे रघुकुल की मान-मर्यादा की पूर्णत: रक्षा करते हैं तथा अपने माता-पिता व गुरुजनों की हर आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। उनके इन्हीं गुणों के कारण ननिहाल में भरत दूत से पूछते हैं-
रघुकुल के आदर्श जिन्हें लगते हैं प्यारे ।
कहो कुशल से तो हैं भ्राता राम हमारे।

(4) द्वेषभाव से रहित–यद्यपि राम को वन भेजने में कैकेयी का ही प्रमुख हाथ रहा है, फिर भी राम को कैकेयी के प्रति कहीं तनिक भी रोष नहीं है, अपितु वे कैकेयी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं
माँ ने नारी को अमरत्व प्रदान किया है।
मोड़ा है इतिहास, नया आदर्श दिया है ।
(5) शक्ति-शील-सौन्दर्य समन्वित-राम शक्तिशाली होने के साथ-साथ शील और सौन्दर्य (UPBoardSolutions.com) से युक्त एक ऐसे महामानव हैं, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति जन-सेवा के लिए ही समर्पित कर दी है, तभी तो . कैकेयी उनके सम्बन्ध में कहती है
राम हमारा शक्ति, शील, सौन्दर्य समन्वित
उसका जीवन ही जन-सेवा हेतु समर्पित।
(6) दीन-रक्षक और दुष्ट संहारक—राम दीन-हीन व्यक्तियों की सदैव सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जहाँ वे असहायों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं वहीं दुष्टों के लिए वे काल के समान हैं। उनके इस रूप को कैकेयी निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करती है-
दुःखी जनों को देख नयन उनके भर आते,
देख दुष्ट को लाल वही लोचन हो जाते ॥
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ‘कर्मवीर भरत’ खण्डकाव्य के राम एक आदर्श और (UPBoardSolutions.com) मर्यादापुरुषोत्तम चरित्र के धारक हैं।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 कर्मवीर भरत (खण्डकाव्य) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Hindi Chapter 1 कर्मवीर भरत (खण्डकाव्य), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
![]()
![]()
![]()