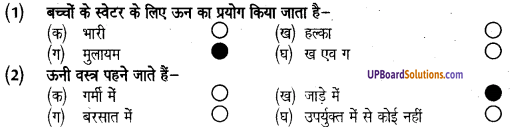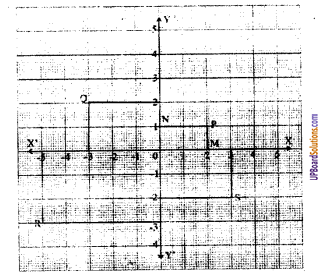UP Board Solutions for Class 6 Hindi Chapter 13 आल्हा-ऊदल (महान व्यक्तिव)
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 6 Hindi. Here we have given UP Board Solutions for Class 6 Hindi Chapter 13 आल्हा-ऊदल (महान व्यक्तिव)
पाठ का सारांश
आल्हा और ऊदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह एवं माता का नाम देवल था। देशराज के एक और सगे भाई वत्सराज थे। माड़वगढ़ की लड़ाई में माड़वगढ़ के राजा कलिंगराय ने धोखे से रात्रि में दोनों भाइयों देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और दोनों की नृशंस हत्या कर दी। उस समय आल्हा और ऊदले दोनों बहुत (UPBoardSolutions.com) छोटे थे। पिता की युद्ध में मृत्यु के बाद आल्हा और ऊदल का पालन-पोषण महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हना द्वारा किया गया। किशोरावस्था में आते-आते दोनों भाई बरछी, बाण, कृपाल एवं घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए।
एक दिन अचानक ऊदल को अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला कि उनकी हत्या की गई थी। आक्रोशित ऊदल ने माता देवल से सच्चाई जाननी चाही। माता ने अपने पुत्रों को युद्ध से बचाने के लिए पिता की बीमारी से मृत्यु होने की बात बताई थी। ऊदल के बार-बार पूछने पर विवश होकर माता ने पिता की हत्या का सारा वृतांत सुनाया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊदल ने अपने बड़े भाई आल्ही के साथ महोबा की सेना लेकर माड़वगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दोनों भाइयों ने युद्ध में पिता के हत्यारे और माड़वगढ़ के राजा । कलिंगराय को पराजित कर दिया। कलिंगराय द्वारा क्षमा माँगने पर दोनों भाइयों ने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार कराई।
दोनो भाइयों की वीरता पर लिखी गई पुस्तक आल्हखण्ड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा धीर-वीर एवं ओजस्वी थे। ऊदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोबा पर आक्रमण के समय हुए भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए। (UPBoardSolutions.com) अब आल्हा का मन निराशा से भर गया। युद्ध के बाद आल्हा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया।
![]()
अभ्यास
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –
प्रश्न 1.
आल्हा-ऊदल के पिता देशराज की हत्या किसने की?
उत्तर :
आल्हा-ऊदल के पिता देशराज की हत्या माड़वगढ़ के राजा कलिंगराय ने की।
प्रश्न 2.
ऊदल और अभय सिंह में द्वंद्व युद्ध क्यों हुआ?
उत्तर :
ऊदल द्वारा राजा माहिल के राज्य की सीमा के भीतर घुसकर हिरण का शिकार करने के कारण राजा माहिल के पुत्र अभय सिंह के साथ ऊदल का द्वंद्व युद्ध हुआ।
प्रश्न 3.
ऊदले को कैसे पता चला कि उनके पिता की हत्या हुई है?
उत्तर :
राजा माहिल के पुत्र अभय सिंह के द्वंद्व युद्ध में ऊदल द्वारा पराजित होने के बाद राजा माहिल आग बबूला हो गए। उन्होंने ऊदल के संरक्षक महोबा के शासक परमाल से ऊदल की धृष्ठता की शिकायत (UPBoardSolutions.com) करते हुए व्यंग किया कि यदि ऊदल इतना बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारे से बदला क्यों नहीं लेता? तब ऊदल को पता चला कि उसके पिता की हत्या हुई थी।
![]()
प्रश्न 4.
माड़वगढ़ की लड़ाई का क्या परिणाम हुआ?
उत्तर :
माड़वगढ़ की लड़ाई में आल्हा और ऊदल ने माड़गढ़ के राजा कलिंगराय को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई।
प्रश्न 5.
हृदय परिवर्तन के बाद आल्हा ने क्या किया?
उत्तर :
हृदय परिवर्तन के बाद आल्हा ने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया।
प्रश्न 6.
आल्हा ऊदल की वीरता को अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर :
आल्हा और ऊदल दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा धीर-वीर एवं ओजस्वी थे। ऊदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। ‘आल्हखंड’ में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। दोनों ही बहादुर और वीर योद्धा थे।
![]()
We hope the UP Board Solutions for Class 6 Hindi Chapter 13 आल्हा-ऊदल (महान व्यक्तिव) help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 6 Hindi Chapter 13 आल्हा-ऊदल (महान व्यक्तिव), drop a comment below and we will get back to you at the earliest.