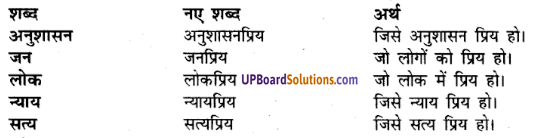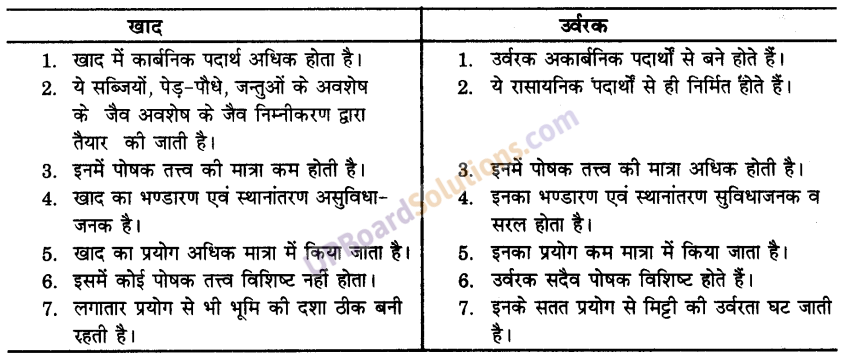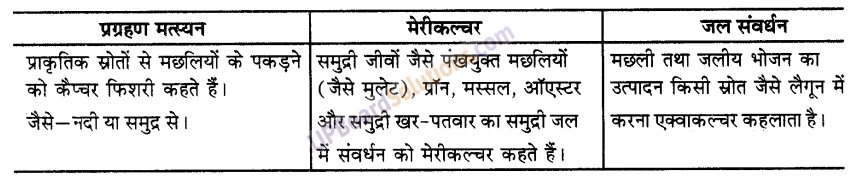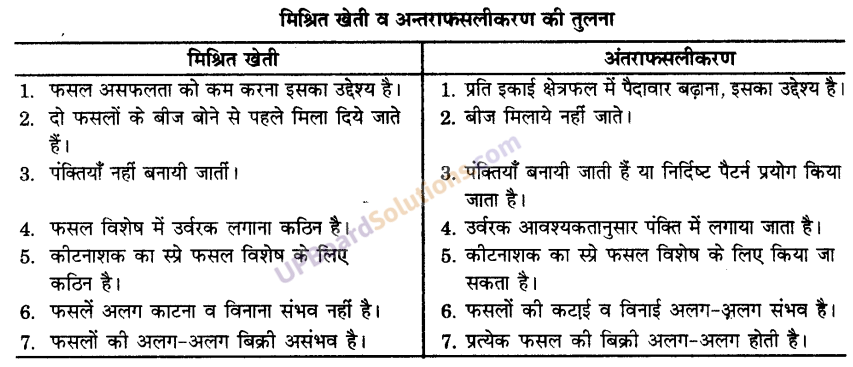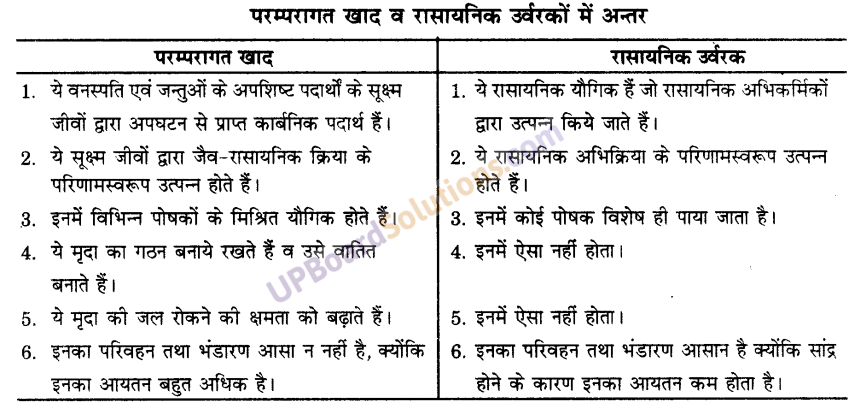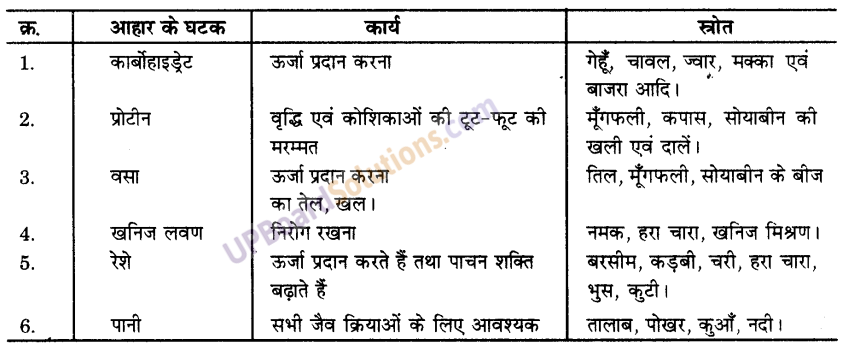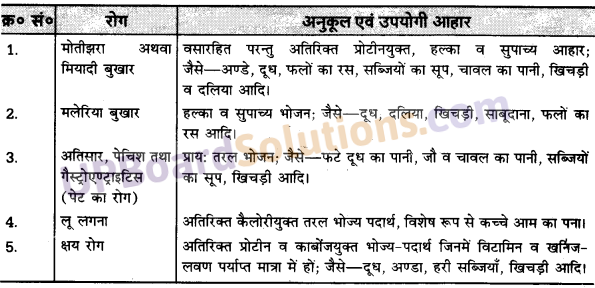UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 15 भोजन पकाना और परोसना तथा तत्त्वों की सुरक्षा
These Solutions are part of UP Board Solutions for Class 10 Home Science . Here we have given UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 15 भोजन पकाना और परोसना तथा तत्त्वों की सुरक्षा.
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1:
भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आप भोजन पकाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखेंगी? [2009, 10, 11, 13, 14]
या
भोजन पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि भोजन के तत्त्व नष्ट न हो सकें ? [2008]
या
भोजन पकाकर खाना क्यों आवश्यक है ? [2016, 37, 18]
या
भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं ? पौष्टिक तत्त्वों की उन पकाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? [2016]
या
पाक-क्रिया के लाभ या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। [2018]
उत्तर:
भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य
आदि-मानव क्षुधापूर्ति के लिए तत्कालीन भोज्य-पदार्थों का प्राकृतिक रूप में ही उपयोग करता था। उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे शिकार करने के लिए अस्त्रों, अग्नि तथा नाना प्रकार के भोज्य-पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कराया। वह धीरे-धीरे अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने में करने लगा। आहार एवं पोषण-विज्ञान के विकास एवं अध्ययन ने आधुनिक मानव को भोजन को पकाने के महत्त्व तथा इसकी वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता की शिक्षा दी है। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं
(1) भोज्य-पदार्थों को सुपाच्य बनाना:
आहार को ग्रहण करने से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि उसका अच्छी प्रकार से पाचन हो जाए। पाक-क्रिया या भोजन को पकाने का एक मुख्य उद्देश्य भोज्य-पदार्थों को सुपाच्य बनाना होता है। बिना पकाए भोज्य-पदार्थों को यदि (UPBoardSolutions.com) ग्रहण किया जाता है, तो इस दशा में उनका पाचन प्रायः असम्भव ही होता है। अतः भोज्य-पदार्थों को सुपाच्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें अनिवार्य रूप से पकाया जाता है।
(2) आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना:
पाक-क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना भी है। विभिन्न खाद्य-सामग्रियाँ कच्ची अवस्था में स्वादिष्ट नहीं होतीं, बल्कि उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है। इन खाद्य-सामग्रियों को यदि सही पाक-क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये स्वादिष्ट बन जाती हैं तथा रुचिपूर्वक खाई जा सकती हैं।

(3) आकर्षक बनाना:
खाद्य-सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की मनभावन सुगन्ध उत्पन्न हो जाती है। अनेक खाद्य व्यंजनों को मसालों एवं रंगों से विशेष आकर्षक बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए-चावल से जब पुलाव या बिरयानी तैयार की जाती है, तो उसमें एक मनोहारी सुगन्ध उत्पन्न हो जाती है तथा उसका रूप भी आकर्षक हो जाता है।
(4) आहार को विविधता प्रदान करना:
पाक-क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य-सामग्री को विविधता प्रदान करना भी है। पाक-क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न-भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आहार की विविधता व्यक्ति को अधिक सन्तोष प्रदान करती है। तथा आहार के प्रति रुचि बनी रहती है।
(5) खाद्य-सामग्री को कीटाणुरहित बनाना:
विभिन्न शाक-सब्जियों तथा भोज्य-पदार्थों पर नाना प्रकार के फफूद एवं जीवाणु होते हैं। वर्षा ऋतु में तो इनकी संख्या अत्यधिक होती है। बिना पके भोज्य-पदार्थों का सेवन करने से ये कीटाणु शरीर में प्रवेश करके अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। भोज्य-पदार्थों को पकाते समय उच्च ताप पर ये कीटाणु लगभग समूल नष्ट हो जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भोज्य-पदार्थों को पकाने का एक उद्देश्य आहार को कीटाणुरहित बनाना भी होता है। जीव जगत से प्राप्त भोज्य सामग्री (दूध, मांस-मछली एवं अण्डे) में कीटाणुओं की अधिक आशंका रही है अतः इन्हे आहार के रूप में ग्रहण करने से पूर्व उच्च ताप पर पकाना अति आवश्यक होता है।
(6) आहार का संरक्षण:
खाद्य-सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना भी है। कच्ची खाद्य-सामग्री शीघ्र ही सड़ने लगती है, परन्तु समुचित पाक-क्रिया द्वारा तैयार खाद्य-सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती है। उदाहरण के लिए-अचार, मुरब्बे, जैम, सॉस आदि के रूप में खाद्य-सामग्री (UPBoardSolutions.com) को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार कच्चा दूध शीघ्र ही फट जाता है, परन्तु यदि उसे पका लिया जाए, तो काफी समय तक ठीक हालत में रखा जा सकता है।
भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें
भोजन पकाने से जहाँ एक ओर अनेक ल हैं, वहीं दूसरी ओर लापरवाही व असावधानीपूर्वक भोजन पकाने से अनेक हानियाँ भी सम्भव हैं। उदाहरण के लिए-गलत विधि से भोजन पकाने पर उसके पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। अतः भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए
(1) स्वच्छ एवं कीटाणुरहित भोजन:
भोजन पकाते समय स्वच्छता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि
(क) गन्दे बर्तनों में कीटाणु उपस्थित रहते हैं; अतः भोजन सदैव स्वच्छ बर्तनों में पकाना चाहिए।
(ख) भोजन बनाने में प्रयुक्त पीतल के बर्तन कलई किए हुए होने चाहिए, अन्यथा भोजन के विषैला होने का भय रहता है।
(ग) भोजन बनाते समय गृहिणी के नाखून साफ-स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों की गन्दगी में अनेक कीटाणु होते हैं, जोकि अनेक रोगों को कारण बन सकते हैं।
(घ) खाना पकाते समय गृहिणी को अपने बाल बँधे व कसे हुए रखने चाहिए, ताकि उनके भोजन में गिरने की सम्भावना ही न रहे।
(ङ) रसोईघर में बर्तन पोंछते समय स्वच्छ कपड़ा प्रयुक्त करना चाहिए।
(2) स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन:
भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है; अत:
(क) भोजन को पकाते समय बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रहने से भोजन वायु के सम्पर्क में आता है, जिससे इसमें कीटाणुओं व धूल गिरने की सम्भावना बनी रहती है तथा भोजन की सुगन्ध भी कम हो जाती है।
(ख) निश्चित अवधि से अधिक देर तक पकाने से भोजन का स्वाद नष्ट हो जाता है तथा उसके पोषकतत्त्वों के नष्ट होने की भी सम्भावना रहती है। अत: खाद्य-सामग्री को केवल उतने ही समय तक पकाना चाहिए जितना आवश्यक हो।।
(ग) भोजन को बार-बार गर्म करने से उसके पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
(घ) खाने का सोडा विटामिन ‘बी’ को नष्ट करता है; अत: इसका उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए।
(ङ) चावल व शाक-सब्जियों को पकाते समय उनमें अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। इनके पानी में पोषक तत्त्व होते हैं; अतः इसे फेंकना नहीं चाहिए।
(च) आवश्यकता से अधिक मसालों का उपयोग करने से भोजन का स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो जाता है तथा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
(छ) सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही काटना चाहिए। छीलने एवं काटने के बाद नहीं । धोना चाहिए। इससे कुछ पोषक तत्त्व पानी में बह जाते हैं।

प्रश्न 2:
जल, भाप, चिकनाई तथा वायु के माध्यम से की जाने वाली पाक-क्रिया की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
या
भोजन बनाने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन कीजिए। [2007, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
या
भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। [2010, 11, 16, 17, 18]
या
भोजन के पोषक तत्वों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भोजन पकाने की विधियाँ लिखिए। [2007, 09, 10, 13, 16]
या
भोजन पकाना क्यों आवश्यक है? भोजन पकाने की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन सी हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम विधि कौन-सी है? वर्णन कीजिए। [2008, 10, 11, 12, 14]
या
भोजन पकाने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। इनके गुण व दोष लिखिए। [2007, 09]
या
जल के माध्यम से भोजन पकाने की दो विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।[2016]
या
भाप से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य क्यों होता है? [2018]
या
तलने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। [2018]
उत्तर:
भोजन पकाना
भोजन को स्वादिष्ट, कीटाणुरहित व सुपाच्य बनाने की दृष्टि से भोजन को पकाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आहार को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए भी उसे पकाकर रखना जरूरी है। कच्ची खाद्य-सामग्री जल्दी ही सड़ने या गलने लगती है।
भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ
सभ्यता एवं आहार सम्बन्धी ज्ञान के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने पाक-क्रिया अर्थात् भोज्यपदार्थों को पकाने की विभिन्न विधियों को भी खोज लिया है। अब भिन्न-भिन्न भोज्य पदार्थों से भिन्नभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसके लिए भिन्न-भिन्न विधियों को भी अपनाया जाता है। यह सत्य है कि भोजन पकाने की प्रत्येक विधि में ताप की आवश्यकता होती है। ताप प्रत्येक पाक-क्रिया का एक आवश्यक कारक होता है, परन्तु (UPBoardSolutions.com) पाक-क्रिया में ताप के अतिरिक्त एक अन्य कारक भी आवश्यक होता है। यह कारक होता है-पाक-क्रिया का माध्यम अर्थात् खाद्य-सामग्री को किस माध्यम से पकाया जाता है। यह माध्यम जल, वाष्प, चिकनाई (तेल या घी) तथा वायु में से कोई भी एक हो सकता है। इन माध्यमों के आधार पर ही पाक-क्रिया की विभिन्न विधियों का निर्धारण होता है। इस प्रकार भोज्य सामग्री को पकाने की विधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जाता है

- जल के माध्यम से पकाना,
- वाष्प के माध्यम से पकाना,
- चिकनाई के माध्यम से पकाना तथा
- वायु के माध्यम से पकाना।
पाक-क्रिया की इन चारों विधियों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है
(1) जल के माध्यम से पकाना:
इस विधि में गर्म जल में भोजन को पकाया जाता है। इसे दो प्रकार से पकाया जा सकता है-..
(क) उबालकर पकाना:
यह भोजन पकाने की अत्यन्त प्राचीन एवं सरल विधि है। पकाये जाने वाले भोज्य-पदार्थों को किसी भगोने अथवा डेगची में पानी डालकर चूल्हे अ थवा अँगीठी पर चढ़ा दिया जाता है। उबलने पर पानी का ताप लगभग 100° सेण्टीग्रेड रहता है। कुछ समय बाद भोजन पकाना और परोसना तथा तत्त्वों की सुरक्षा 211 भोज्य पदार्थ भली प्रकार गल जाते हैं। इस विधि द्वारा प्राय: दालें व चावल तथा आलू, अरवी व इसी प्रकार की अन्य सब्जियाँ पकाई जाती हैं। सब्जियों को छिलके सहित उबालकर पानी फेंक देने से इनके पोषक तत्त्व नष्ट नहीं होते, परन्तु चावल पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए तथा पकने के बाद पानी को फेंकना नहीं (UPBoardSolutions.com) चाहिए क्योंकि इसमें पोषक तत्त्व विद्यमान रहते । हैं। उबालकर पकाया गया भोजन हल्का, सुपाच्य व गुणवत्तापूर्ण होता है।

(ख) धीमी आँच पर पकाना:
इसमें भोज्य-पदार्थों को मसालों सहित थोड़े पानी में डालकर मन्द आँच (लगभग 82° सेण्टीग्रेड) पर पकाया जाता है साबुत दाल, सब्जियाँ व मांस आदि पकाने की यह एक उत्तम विधि है। जिनमें भोजन के पोषक तत्त्व नष्ट नहीं होते तथा भोजन भी सुपाच्य एवं स्वादिष्ट बनती है।
(2) वाष्प के माध्यम से पकाना:
भोजन पकाने की यह एक आधुनिक विधि है जिसमें भोजन के अधिकांश पौष्टिक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह भगोने के आकार का होता है जिसमें थोड़े से पानी के साथ भोज्य-पदार्थ डालकर वायु अवरोधक ढक्कन लगा दिया जाता है। इसे अँगीठी अथवा गैस बर्नर पर रखने से पानी गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप के दबाव व ताप के द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में भोजन पक जाता है। विभिन्न प्रकार की दालें, सब्जियाँ व मांस आदि पकाने की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में ईंधन व समय की बचत होती है, भोजन के पोषक तत्त्व नष्ट नहीं होते तथा भोजन स्वादिष्ट एवं सुपाच्य बनता है।
(3) चिकनाई के माध्यम से पकाना:
इस विधि में भोजन पकाने के लिए तेल व घी को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तेल (UPBoardSolutions.com) अथवा घी में भोज्य पदार्थों को पकाने की विधि को तलना कहते हैं। भोज्य-पदार्थों को तलने की निम्नलिखित तीन विधियाँ प्रचलित हैं।

(क) उथली विधि:
इस विधि में चौड़ी व उथली कड़ाही अथवा तवे को प्रयोग में लाया जाता है। कड़ाही में थोड़ा तेल अथंवा घी डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया जाता है। घी अथवा तेल के अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इसमें भोज्य पदार्थों को तला जाता है। आलू की टिकिया, कटलेट्स, पराँठे, चीले, आमलेट इत्यादि इसी विधि से बनाए जाते हैं। कई बार इस विधि से मसाला डोसा जैसे व्यंजन तलने के लिए कड़ाही के स्थान पर सपाट तवे का प्रयोग किया जाता है।

(ख) गहरी विधि:
इस विधि में गहरी कड़ाही प्रयोग में लाई जाती है। कड़ाही में तेल अथवा घी पर्याप्त मात्रा में डालकर उसे खौलने तक गर्म (लगभग 175°सेण्टीग्रेड ताप) किया जाता है। अब भोज्य-पदार्थों को इसमें अच्छी प्रकार तला जाता है। इस विधि से प्रायः सभी प्रकार के पकवान; जैसे-पूड़ी-कचौड़ी, समोसे, पकौड़ियाँ तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ इत्यादि बनाए जाते हैं। तलने की विधि द्वारा भोजन (पकवान) पकाने की विधि अत्यन्त प्राचीन है। इसकी अपनी लोकप्रियता (UPBoardSolutions.com) अलग ही प्रकार की है। इस विधि से भोजन स्वादिष्ट तो बनता है, परन्तु गरिष्ठ होने के कारण सुपाच्य नहीं होता।
(ग) शुष्क विधि:
इस विधि द्वारा केवल कुछ विशेष प्रकार की खाद्य सामग्री को ही पकाया जा सकता है। कुछ खाद्य-सामग्री ऐसी होती है जिनमें से ताप पाकर स्वतः ही चिकनाई निकलती है। उदाहरण के लिए-चर्बीयुक्त सूअर का मांस या बेकन आदि। इन खाद्य-सामग्रियों को तलने के लिए अतिरिक्त चिकनाई की आवश्यकता नहीं होती।
ध्यान रखने योग्य बातें:
चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने या तलने के समय कुछ बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। कड़ाही में घी या तेल डालकर तब तक गर्म करना चाहिए, जब तक उसमें से कुछ-कुछ धुआँ-सा न उठने लगे तब उसमें तलने वाली सामग्री डालनी चाहिए। इस सामग्री को हिलाते तथा उलटते-पलटते रहना चाहिए। समुचित ढंग से पक जाने पर सामग्री को निकाल लेना चाहिए। निकालकर कुछ समय तक उसे पोनी में ही रखना चाहिए, जिससे कि फालतू घी या तेल निकल जाए। तलते समय सामग्री के छोटे-छोटे टुकड़े टूट-टूटकर घी में गिरते रहते हैं। इन्हें मुख्य सामग्री के साथ-साथ निकालते रहना चाहिए अन्यथा ये जल कर अप्रिय गन्ध छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त तलते समय इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि गर्म घी या तेल में पानी के छींटे न पड़े। इससे गर्म घी छिटक कर, तलने वाले के शरीर पर पड़ सकता है।
(4) वायु के माध्यम से पकाना:
वायु अग्नि प्रज्वलित करती है तथा अग्नि के सम्पर्क में आकर स्वयं भी गर्म हो जाती है। वायु का यह गुण ही भोजन पकाने की इस विधि का आधार है। वायु द्वारा भोजन पकाने की प्रचलित विधियाँ निम्नलिखित हैं

(क) भूनना (रोस्टिग):
इस विधि के अन्तर्गत बालू या राख को गर्म करके उसमें सम्बन्धित वस्तु को भून कर पकाया जाता है। इस विधि से बैंगन आदि का भुर्ता बनाया जा सकता है। आलू, शंकरकन्द, मक्का, बाजरा या चने आदि भूने जा सकते हैं। इस प्रकार से भूनी हुई वस्तुएँ काफी स्वादिष्ट व पाचक होती हैं। किसी प्रकार की चिकनाई आदि का प्रयोग न होने के कारण ये सामग्री सुपाच्य होती है।
(ख) सेंकना:
सामान्य रूप से भूनना एवं सेंकना एक ही समझा जाता है, परन्तु वास्तव में इन दोनों क्रियाओं में पर्याप्त । अन्तर है। सेंकने की क्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित खाद्य-सामग्री को आग के सम्पर्क में लाया जाता है। सामान्य रूप से धुआँरहित, जलते हुए अंगारों पर वस्तुओं (UPBoardSolutions.com) को सेंका जाता है। भुट्टे, कबाब
आदि इसी विधि से सेंके जाते हैं।

(ग) तन्दूर अथवा भट्टी में पकाना (बेकिंग):
रोटी, डबलरोटी, बन व बिस्कुट आदि इस विधि द्वारा ही पकाये जाते हैं। चित्र 15.4-सेंकना मिट्टी का बना हुआ तन्दूर रोटी सेंकने के लिए तथा ओवन अथवा विशिष्ट भट्टी में बिस्कुट, डबल रोटी, बन, पेस्टी, नानखताई आदि पकाए जाते हैं।
पाक-क्रिया की सर्वोत्तम विधि
भाप देकर भोजन पकाने की कुकर्स की विधि बहुत अच्छी है। इस रीति से भोजन पकाने में पौष्टिक तत्त्व नष्ट नहीं होने पाते तथा हल्के व सरलता से पंचने योग्य हो जाते हैं। इस रीति से कार्य करने में समय कम लगता है। जलने का भय नहीं रहता और ईंधन भी कम मात्रा में व्यय होता है। अतः मितव्ययिता तथा समय की बचत–सभी दृष्टियों से यह विधि श्रेष्ठ है।
प्रश्न 3:
भोजन परोसने की शैलियों का वर्णन करते हुए अपनी दृष्टि में उपयुक्त शैली का उल्लेख कीजिए। [ 2007, 08,10,11]
या
भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आवश्यक हो तो चित्र भी बनाइए।
या
“भोजन परोसना एक-कला है।” स्पष्ट कीजिए। भोजन परोसने की देशी, विदेशी विधियों के बारे में भी लिखिए। [2018, 10, 11]
या
भोजन परोसने की देशी व विदेशी शैली में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [2016]
या
भोजन परोसना एक कला है। क्यों ? [2011, 14]
या
भोजन परोसने की कौन-सी विधियाँ हैं? भारतीय ढंग से भोजन परोसने की विधि लिखिए। [2015, 16 ]
उत्तर:
भोजन परोसना
पौष्टिक भोजन तैयार करना गृहिणी का एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है, परन्तु परिवार के सदस्यों एवं अतिथियों की भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी गृहिणी का उतना ही महत्त्वपूर्ण दायित्व है। अतः भोजन परोसना पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के समान (UPBoardSolutions.com) ही महत्त्व रखता है। इसके लिए गृहिणी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- भोजन परोसने वाले का व्यवहार विनम्र, मनोहारी तथा कुशल होना चाहिए।
- भोजन परोसने का स्थान व बर्तन स्वच्छ होने चाहिए।
- भोज्य-पदार्थों को विधि के अनुसार उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए।
- भोजन परोसने के स्थान अथवा मेज पर फूलदान व अन्य अनेक प्रकार की कलात्मक सजावट करने से भोजन के आकर्षण में कई गुना वृद्धि हो जाती है। । उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भोजन परोसना एक कला है, जो कि भोजन के प्रति रुचि एवं आकर्षण में वृद्धि करती है।
भोजन परोसने की विभिन्न शैलियाँ (विधियाँ)
प्रायः भोजन परोसने की तीन निम्नलिखित शैलियाँ (विधियाँ) प्रचलित हैं
(क) देशी शैली,
(ख) विदेशी अथवा पाश्चात्य शैली तथा
(ग) बुफे शैली।
(क) देशी शैली :
यह अति प्राचीन भारतीय शैली है जिसमें भोजन ग्रहण करने वालों के लिए भूमि पर आसन बिछाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अलग थाली में भोजन परोसा जाता है। थाली में शुष्क भोज्य-पदार्थ तथा कटोरियों में तरल भोज्य-पदार्थ परोसे जाते हैं। प्रारम्भ में थोड़ी मात्रा में भोजन परोसा जाता है तथा फिर भोजन ग्रहण करने वाले की आवश्यकतानुसार और भोजन परोसा जाता है।
विशेषताएँ:
देशी शैली में भोजन परोसने की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
- भोजन परोसते समय प्रत्येक खाद्य-पदार्थ के लिए अलग-अलग चम्मच, चमचा व कल्छी आदि होने चाहिए।
- प्रथम बार कम भोजन परोसना चाहिए तथा फिर खाने वालों से पूछ-पूछ कर विभिन्न खाद्य पदार्थ परोसने चाहिए। इससे भोजन व्यर्थ नहीं जाता।
- तरल पदार्थों को कटोरियों में ही परोसना चाहिए।
- थाली में चपातियाँ, पूड़ी व चावल आदि अलग-अलग परोसे जाने चाहिए।
- भोजन का स्थान व बर्तन स्वच्छ होने चाहिए।
- भोजन परोसने से पूर्व गृहिणी को स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए।
(ख) विदेशी अथवा पाश्चात्य शैली:
यह शैली परम्परागत शैली से सर्वथा विपरीत है। इस शैली में भोजन एक विशिष्ट मेज (डाइनिंग टेबल) पर परोसा जाता है तथा खाने वाले कुर्सियों (डाइनिंग चेयर्स) पर बैठते हैं। इस शैली में भोजन एक ही बार में परोस दिया जाता है। इस शैली की अन्य विशिष्ट बातें हैं
- मेज के केन्द्र में प्लेट में चपातियाँ, एक विशिष्ट रचना की प्लेट (राइस प्लेट) में चावल तथा डोंगों में सब्जियाँ प्रायः एक ही बार में परोस दी जाती हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, छुरी, काँटा तथा चम्मच रखी जाती है।
- तरल पदार्थों के लिए बाउल प्रयुक्त किए जाते हैं। बाउल को प्लेट के दाईं (UPBoardSolutions.com) ओर रखना चाहिए।
- छुरी, प्लेट के दाईं ओर तथा उसकी धार प्लेट की ओर होनी चाहिए। काँटा प्लेट के बाईं ओर रखा जाना चाहिए।
- मेज पर आवश्यकतानुसार मसालेदानियाँ, अचार वे मुरब्बे आदि केन्द्रीय भाग में रखे जा सकते हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस विधि में गिलास में सजाकर एक नेपकिन भी रखा जाता है।

(ग) बुफे शैली:
भोजन करने वालों की संख्या अधिक होने पर प्रायः इस शैली को प्रयोग में लाया जाता है। सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि बड़ी दावतों के लिए यह एक सर्वोत्तम आदर्श विधि है। इस विधि में. एक बड़े हॉल अथवा पंडाल में एक ओर लम्बी मेजें लगा दी जाती हैं। इन्हें विधिपूर्वक सजाया जाता है। मेजों पर निश्चित दूरियों पर प्लेटें, छुरियाँ, काँटे व चम्मच आदि सेट कर रख दिए जाते हैं। प्रत्येक सेट के पास में डोंगों में सब्जियाँ तथा अलग-अलग प्लेट में चपातियाँ, पूड़ियाँ, चावल आदि रख दिए जाते हैं। पंडाल के एक कोने में जल की व्यवस्था कर दी जाती है। बुफे शैली में भोजन औपचारिक, अर्द्ध-औपचारिक तथा अनौपचारिक विधि से परोसा जाता है। औपचारिक ढंग में अतिथि स्वयं खाना परोसकर एक ओर खड़े होकर खाते हैं। अर्द्ध-औपचारिक विधि में मेजबान अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों के सहयोग से अतिथियों को भोजन परोसता है। (UPBoardSolutions.com) अनौपचारिक विधि में वेटर अतिथियों को
भोजन परोसते हैं।
विशेषताएँ: इस प्रकार इस शैली में
(1) अतिथि खड़े होकर भोजन करते हैं।
(2) अतिथियों की संख्या अधिक होती है।
(3) मेजों की एक लम्बी कतार की व्यवस्था में भोजन प्रायः एक से अ सेटों में सजाकर एक साथ परोसा जाता है।
(4) सामान्यतः अतिथि अपने लिए स्वयं ही भोजन परोसते हैं।
प्रश्न 4:
खाद्य-पदार्थों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य-पदार्थों के संरक्षण के कतिपय उपायों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
खाद्य-पदार्थों का संरक्षण व उसके लाभ
खाद्य-पदार्थों को एक लम्बी अवधि तक फफूदी एवं जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधियों को खाद्य-पदार्थों का संरक्षण कहते हैं। इससे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं
- प्रायः गृहिणियाँ फसल के समय पूरे वर्ष के लिए सस्ता अनाज खरीदकर रख लेती हैं। यदि यह अनाज संग्रह काल में सुरक्षित रहे, तो गृहिणी को धन की पर्याप्त बचत होती है तथा उसे अनाज खरीदने के लिए बार-बार बाजार जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
- मौसम की सब्जियों को यदि सुरक्षित रूप से संगृहीत कर लिया जाए, तो उन्हें विपरीत मौसम में उपयोग में लाया जा सकता है।
- महँगे भोज्य-पदार्थों के शेष बचकर व्यर्थ होने पर पर्याप्त आर्थिक हानि होती है जिसका निराकरण खाद्य-संरक्षण के उपाय अपनाकर किया जा सकता है। संरक्षण की विधियाँ
प्रमुख खाद्य-पदार्थों के संरक्षण की प्रचलित विधियाँ निम्नलिखित हैं
(1) स्वच्छता से संग्रह करके:
प्रायः गन्दे स्थानों व बर्तन आदि में फफूदी व जीवाणुओं की उपस्थिति की सम्भावना अधिक रहती है; अत: भोज्य पदार्थों का संग्रह स्वच्छ स्थान एवं स्वच्छ बर्तनों में करना चाहिए।
(2) सुखाकर:
नमी व सीलन में फफूदी व जीवाणु आसानी से पनपते हैं। अतः खाद्य-पदार्थों को शुष्क स्थान में रखना चाहिए। कुछ खाद्य-पदार्थ; जैसे- आलू, मेथी, गाजर, पोदीना, मटर, चना, फल व मेवे आदि; शुष्क अवस्था में हर प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। मटर, चना, गोभी आदि को तो सामान्यतः शुष्कीकरण या निर्जलीकरण (डी-हाइड्रेशन) द्वारा पूर्णरूप से जलरहित कर डिब्बों आदि में बन्द कर संगृहीत कर लिया जाता है तथा विपरीत मौसम में इन सब्जियों का आनन्द लिया जाता है।
(3) उबालकर:
अनेक खाद्य-पदार्थों को उबालकर जीवाणुरहित कर लिया जाता है। अब इन्हें वायुरोधक डिब्बों में भरकर काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
(4) चाशनी में रखकर:
अनेक फलों को शक्कर की चाशनी में पकाकर मुरब्बों के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।
(5) अचार, सॉस आदि बनाकर:
प्रायः सभी घरों में आम, गोभी, गाजर, मिर्च आदि का अचार डाला जाता है, जो कि एक लम्बी अवधि तक सुरक्षित रहता है। इसका कारण है नमक व सरसों के तेल का प्रयोग जो फफूदी व जीवाणुओं से अचार को सुरक्षित रखते हैं। टमाटर की चटनी व सॉस को सुरक्षित रखने के लिए इनमें उपयुक्त मात्रा में सोडियम बेन्जोएट तथा साइट्रिक अम्ल मिलाना सर्वोत्तम रहता है।
(6) ठण्डा रखकर:
आलू व अन्य अनेक प्रकार की सब्जियों को शीतगृह में सुरक्षित रखना एक लोकप्रिय (UPBoardSolutions.com) व्यापारिक विधि है। इस विधि का प्रयोग घरों में रेफ्रिजेरेटर के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजेरेटर में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, भोज्य सामग्री, दूध, अण्डे व मांस आदि को काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
(7) विकिरण विधि द्वारा:
अनेक खाद्य-पदार्थों को विकिरण उपचार द्वारा जीवाणुरहित कर सुरक्षित रखा जाता है।
(8) अनाजों के संरक्षण की विधि:
अनाजों को प्रायः शुष्क स्थानों पर टंकियों में भरकर रखा जाता है। विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग कर इन्हें घुन जैसे हानिकारक कीड़ों से सुरक्षित रखा जाता है। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा इसे चूहों से बचाना चाहिए।

(9) दुध को सुरक्षित रखने की विधि:
कम ताप पर दूध प्राय: सुरक्षित रहता है। अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसमें दूध को 65° सेण्टीग्रेड ताप पर आधा घण्टा रखकर उसे किसी बोतल अथवा बन्द बर्तन में शीतल स्थान पर रख दिया जाता है।
(10) अण्डा, मांस व मछली को सुरक्षित रखनी:
अण्डे को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए कम तापक्रम ही एकमात्र उपाय है। मांस को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसे सुरक्षित रखने के लिए बर्फ के तापक्रम पर रखना चाहिए। मछली को सुरक्षित रखना कठिन कार्य है। कम ताप पर भी मछली केवल कुछ समय तक ही सुरक्षित रहती है। व्यापारिक स्तर पर मछलियों को शुष्क अवस्था में डिब्बों में बन्द कर सुरक्षित रखा जाता है।
प्रश्न 5:
भोजन में मिलावट से क्या अभिप्राय है? शुद्ध भोजन को किन पदार्थों की मिलावट से अशुद्ध किया जाता है?
या
मिलावटी खाद्य-पदार्थों से क्या हानियाँ होती हैं? मिलावटी पदार्थों से बचने के उपाय बताइए।
उत्तर:
भोजन में मिलावट का अर्थ
खाद्य-पदार्थों में मिलावट का अर्थ है “शुद्ध भोज्य-पदार्थों में अन्य सस्ते खाने या न खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर उनके गुणों में कमी करना या उन्हें हानिकारक बनाना।”
आजकल अधिकांश वस्तुएँ मिलावटयुक्त ही मिल रही हैं। दूध में पानी तथा अनाजों, मसालों में कुछ रासायनिक या वनस्पति पद के छिलके, धूल-गर्द मिलना साधारण-सी बात है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भोज्य-पदार्थों में इतनी मिलावट का कारण क्या है? (UPBoardSolutions.com) इसका एक स्पष्ट कारण विक्रेता द्वारा धन-लाभ को प्राथमिकता दिया जाना है।
मुख्य वस्तुओं के ही दाम पर असली पदार्थों के समान रूप-गुण वाली सस्ती या खराब वस्तुएँ बेचने के लिए उन्हें मुख्य पदार्थों के साथ मिलाकर बेचा जाता है, अज्ञानतावश लोग उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं, जिससे उसके धन एवं स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। अत: मिलावटी वस्तुओं से बहुत सावधान रहना चाहिए।
मिलावटी वस्तुओं को लोग बड़ी चालाकी से बेचते हैं। फिलहाल तो ब्राण्डेड पैक वस्तुएँ भी बाजार में मिलावटी उपलब्ध हैं। अत: इससे बचने के लिए आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि किन-किन वस्तुओं में प्रायः मिलावट की जाती है।
विभिन्न भोज्य-पदार्थों में मिलावट:
व्यापारी भिन्न-भिन्न खाद्य-पदार्थों में निम्न प्रकार की सस्ती व हानिकारक वस्तुओं की मिलावट करते हैं
- अनाज: सस्ते व सड़े-गले अनाज, कंकड़, मिट्टी तथा टूटे हुए अनाज।
- आटा, मैदा: पुराना सड़ा आटा या मैदा कभी-कभी खड़िया मिट्टी।
- घी: वनस्पति घी, चर्बी।
- दूध: पानी, अरारोट, अन्य पशुओं का दूध मिलाना अथवा उसमें से वसा निकाल लेना। अब तो यूरिया, रिफाइण्ड तेल आदि से सिन्थेटिक दूध भी तैयार किया जाने लगा है, जिसे दूध में मिलाकर बेचा जा रहा है।
- तेल: अखाद्य-पदार्थों; जैसे–अरण्डी आदि का तेल मिलाना।
- टमाटर की चटनी (Sauce) में कद्दू या अन्य सड़ी सब्जी का प्रयोग।
- काली मिर्च: पपीते के बीज।
- लौंग: तेल निकाल कर सुकड़ी हुई छोटी-छोटी लौग मिलाना।
- जीरा: जीरे के पौधे का बीज, कंकड़, मिट्टी या सीके मिलाना।
- पिसा धनिया: धनिये की भूसी, राँगा हुआ लकड़ी का बुरादा, घोड़े की सूखी हुई लीद।
- पिसी लाल मिर्च: गेरु, लाल ईंट का चूरा, सूखी (UPBoardSolutions.com) लाले बेर के छिलके का बुरादा।
- पिसी हल्दी: पीली मिट्टी या रंगा हुआ अरारोट।
- पिसी खटाई: पीली आम की गुठली।
- चाय: प्रयोग की हुई चाय की पत्ती, पुरानी या खराब पत्तियाँ, चाय की पत्ती का चूरा तथा मिट्टी।
- मिठाइयाँ: मैदा, अरारोट, मिलावटी खोया व वर्जित रंग।
- शर्बत: चीनी के बजाय सैक्रीन (एक रासायनिक मीठा पदार्थ)।
- शहद: गुड़ की चाशनी।।
- केसर: पीली रँगी मुँज या भुट्टे के रंगे हुए छोटे-छोटे रेशे।
इस प्रकार उपर्युक्त तरीकों से अनाजों व मसालों में मिलावट करके अपनी अशुद्ध वस्तुओं को बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है।

मिलावटी खाद्य-पदार्थों से हानियाँ
मिलावटी खाद्य-पदार्थों के सेवन से निम्नलिखित हानियाँ होने की प्रबल सम्भावना होती है
- मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते रहने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है।
- मिलावटी व अशुद्ध भोजन से हैजा, पेचिश, गले की खराबियाँ आदि रोग हो सकते हैं।
- खाने वाले रंग कैन्सरं का. कारण भी बन जाते हैं।
- ऐसे भोजन से कभी-कभी ‘फुड प्वायजनिंग’ से लोगों की मृत्यु तक होती देखी जाती है।
- मिलावटी वस्तुएँ खरीदने से क्रेता को निश्चित रूप से आर्थिक लाभ के स्थान पर हानि होती है।
मिलावट से बचाव के उपाय
मिलावट से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जाते हैं
- बाजार के पिसे मसालों की अपेक्षा घर में पिसे मसाले प्रयुक्त कीजिए अथवा चक्की पर पिसवा लीजिए।
- सदैव कम्पनी संस्तुत विश्वसनीय दुकान से ही स्टैण्डर्ड कम्पनी का माल खरीदिए।
- दूध को अपने सामने ही दुहकर लीजिए अथवा विश्वसनीय डेरी से खरीदिए।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1:
पाक-क्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए। [2008, 10]
उत्तर:
प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य-सामग्री को आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए कृत्रिम रूप से तैयार करने की व्यवस्थित क्रिया को ही पाक-क्रिया कहते हैं। पाक-क्रिया के अन्तर्गत प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध खाद्य-सामग्री को जल, ताप, चिकनाई तथा भाप एवं वायु आदि द्वारा ऐसा रूप दिया जाता है जो इस सामग्री को अधिक स्वादिष्ट, नर्म एवं सुपाच्य बना देता है। जब हम किसी सब्जी को लेकर उसे धोते, छीलते एवं काटते हैं या उबालते एवं छोंकते हैं, तब इन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पाक-क्रिया ही कहा जाता है। इसी प्रकार से जब हमें गेहूं को पीसते, आटा गूंथते तथा रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंकते हैं, (UPBoardSolutions.com) तो ये समस्त क्रियाएँ भी पाक-क्रिया की ही उप-क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार पाक-क्रिया अपने आप में एक विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रिया है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण से भी पाक-क्रिया के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रेशर कुकर है।

प्रश्न 2:
तलने के लाभ एवं हानियाँ लिखिए।
उत्तर:
तलने के लाभ-तलकर भोजन पकाने के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं
- तलकर पकाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट एवं रुचिकर होता है।
- तले हुए भोजन में एक प्रकार की मनमोहक सुगन्ध एवं आकर्षक रंग आ जाता है, जिसका खाने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
- तलकर पकाया गया भोजन खा लेने के बाद काफी समय तक पुनः भूख नहीं लगती।
तलने की हानियाँ:
तलकर भोजन बनाने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं
- चिकनाई के माध्यम से तलकर पकाया गया भोजन गरिष्ठ हो जाता है तथा शीघ्र नहीं पचता।
- तल कर पकाए गए भोजन के विटामिन तथा कुछ पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
- अधिक तला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे पेट व गले में जलन हो सकती है।
प्रश्न 3:
पाक-क्रियाओं का पौष्टिक तत्त्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? [2011]
या
प्रोटीन पर पाक-क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। [2014]
उत्तर:
प्रोटीन पर पकाने का प्रभाव:
जन्तुजन्य प्रोटीन पकाने पर प्रायः कठोर हो जाने के कारण सुपाच्य नहीं रहती। वनस्पतिजन्य प्रोटीन पकाने पर कोशा-भित्तियों से बाहर आ जाती है; अतः अधिक सुपाच्य हो जाती है। भोज्य-पदार्थों को तलकर पकाने से उनमें उपस्थित प्रोटीन अत्यधिक कड़ी तथा अपाच्य हो जाती है; अत: प्रोटीनयुक्त भोज्य-पदार्थों को तलना नहीं चाहिए।
विटामिन पर पकाने का प्रभाव:
विटामिन ‘ए’ व ‘डी’ अत्यधिक उच्च ताप पर नष्ट हो जाते हैं, परन्तु भोज्य-पदार्थों को सामान्य विधि के अनुसार पकाने पर इन विटामिनों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। विटामिन ‘बी’ पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु जल में विलेय होने के कारण भोज्य-पदार्थों (UPBoardSolutions.com) को अधिक पकाने पर इसका कुछ भाग जल के साथ ही नष्ट हो जाता है। सब्जी का हरा रंग बनाये रखने के लिए प्रयुक्त सोडा बाइकार्बोनेट विटामिन ‘बी’ को नष्ट कर देता है। इसलिए हरी सब्जियों को पकाते समय खाने के सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विटामिन ‘सी’ भी जल में घुलनशील होता है तथा उच्च ताप पर यह नष्ट हो जाता है।
नोट- अन्य पोषक तत्त्वों पर पाक-क्रियाओं के प्रभाव का विवरण आगामी प्रश्नों में वर्णित है।

प्रश्न 4:
तरकारियों को छीलने से क्या हानि होती है?
उत्तर:
पाक-क्रिया के लिए तरकारियों को छीला तथा काटा भी जाता है। तरकारियों के छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं। अतः तरकारियों को छीलने से इन पोषक तत्त्वों की हानि होती है, जिनसे बचने के लिए
- तरकारियों को भली प्रकार धोकर छिलकायुक्त ही काटकर पकाना चाहिए। इससे छिलके में उपस्थित पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं।
- मोटे छिलके वाली तरकारियों के छिलके अधिक गहरे नहीं छीलने चाहिए, क्योंकि पोषक तत्त्वों की छिलकों के साथ ही निकल जाने की सम्भावना रहती है।
प्रश्न 5:
पाक-क्रिया का वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है? [2008, 11, 12, 14]
उत्तर:
साधारणतः पाक-क्रिया का वसा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु अधिक ताप पर निरन्तर गर्म करने से वसा का एक नया यौगिक बन जाता है, जिसे एक्रोलीन कहा जाता है। इस यौगिक की एक विशेष गन्ध होती है; अतः इस अवस्था में वसायुक्त भोजन में एक तीखी गन्ध आने लगती है। यह एक्रोलीन नामक यौगिक खाने योग्य नहीं होता। अत: इससे युक्त आहार ग्रहण करने से हानि हो। सकती है। यदि वसायुक्त भोजन को बार-बार गर्म किया जाए तो वह सरलता से पचने योग्य नहीं रह जाता। वसा अधिक ताप के प्रभाव से ग्लिसरॉल तथा स्निग्ध के रूप में विघटित भी हो जाती है।

प्रश्न 6:
पाक-क्रिया का कार्बोहाइड्रेट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
पाक-क्रिया का कार्बोहाइड्रेट्स पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हम भोजन में सामान्य रूप से स्टार्च एवं शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हैं। स्टार्च को जब पकाया जाता है तो वे पककर मुलायम हो जाते हैं तथा कुछ फूल जाते हैं। इस अवस्था में इनका पाचन सरल हो जाता है। यदि स्टार्च को क्वथनांक तक उबाला जाए तो इसका सेल्यूलोज वाला भाग फट जाता है। यदि इस प्रकार से पकते हुए स्टार्च में कुछ मात्रा में ठण्डा पानी मिला दिया जाए तो स्टार्च के कण अलग-अलग हो जाते हैं तथा भोज्य-पदार्थ लेई के समान हो जाता है। इससे भिन्न, यदि स्टार्च को जलरहित ही शुष्क विधि से पकाया जाए, तो स्टार्च का रंग हल्का बादामी हो जाता है। यदि कुछ अधिक ताप पर स्टार्च को गर्म किया जाए, तो उसका रंग काला हो जाता है। ताप पाकर यह स्टार्च डैक्स्ट्रीन का रूप ग्रहण कर लेता है। इस रूप में स्टार्च अधिक सुपाच्य हो जाता है। इसी प्रकार, यदि शर्करा को शुष्क अवस्था में गर्म किया जाए, तो उसका रंग भूरा हो जाता है। परन्तु यदि शर्करा को जल के साथ गर्म किया जाए, तो वह घुल जाती है तथा एक प्रकार से शर्बत का रूप ग्रहण कर लेती है।
प्रश्न 7:
पाक-क्रिया का खनिज-लवणों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
पाक-क्रिया का खनिज-लवण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब विभिन्न खाद्य-सामग्रियों को जल के साथ पकाया जाता है, तो विभिन्न खनिज-लवण जल में आ जाते हैं। इस अवस्था में यदि पकी हुई खाद्य-सामग्री में से अतिरिक्त पानी बहा दिया जाए तो विभिन्न खनिज लवणों के नष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य-सामग्री को केवल उतने ही जल में उबाला जाए जितना पकाने में प्रयुक्त हो जाए। (UPBoardSolutions.com) इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को पकाने से पूर्व अधिक समय तक काटकर नहीं रखना चाहिए। सब्जियों को काटने एवं छीलने से पहले ही अच्छी तरह से धो लेना। चाहिए। छीलकर एवं काटकर धोने से बहुत-से खनिज-लवण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि खाद्य सामग्री को सावधानीपूर्वक पकाया जाए, तो खनिज लवणों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।
प्रश्न 8:
घर में अनाजों की सुरक्षा आप कैसे करेंगी?
उत्तर:
घर में अनाजों की सुरक्ष: के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए
- खुले हुए अनाज को समय-समय पर सुखाना चाहिए।
- अनाजों को घुन, सुरसुरी आदि से बचाने के लिए उसमें कोई दवा; जैसे-गोलियाँ आदि; रखनी चाहिए।
- अनाजों को सीलबन्द बर्तनों में रखना चाहिए विशेषकर धातु के बने ड्रम आदि इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त रहते हैं।
- अनाजों में जल की मात्रा कम-से-कम रहनी चाहिए, ताकि उन पर फफूद, घुन आदि न लग सकें। इसके लिए उन्हें पूर्णतः सूखा हुआ रखना चाहिए।
प्रश्न 9:
सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है? सब्जियों को काटते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? [2009, 10, 11]
उत्तर:
सब्जियाँ हमारे भोजन का अनिवार्य अंग मानी जाती हैं। सब्जियों को सुरक्षात्मक खाद्यसामग्री माना जाता है। सब्जियाँ विभिन्न विटामिन्स एवं खनिज लवणों की उत्तम स्रोत होती हैं। ये विटामिन एवं खनिज-लवण हमारे स्वास्थ्य में विशेष रूप से सहायक होते हैं। सब्जियों में रेशों की भरपूर मात्रा होती है; अतः सब्जियाँ कब्ज-निवारक होती हैं। सब्जियाँ मल-विसर्जन में सहायक होती हैं। सब्जियाँ शरीर में अम्ल एवं क्षार के सन्तुलन को बनाये रखने में सहायक होती हैं। सब्जियाँ भूख बढ़ाती हैं। सब्जियों के समावेश से हमारा भोजन अधिक रुचिकर एवं विविधतापूर्ण बनता है।
सब्जियों को काटते एवं पकाते समय कुछ बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए
- सब्जियों को सदैव अच्छी तरह से धोकर एवं साफ करके ही छीलना या काटना चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो सब्जियों का छिलका नहीं उतारना चाहिए।
- सब्जियों को छीलने एवं काटने के उपरान्त बिल्कुल नहीं धोना चाहिए।
- सब्जियों को सदैव ढककर पकाना चाहिए।
- सब्जियों को केवल उतने ही जल में पकाना चाहिए जितना जल उन्हें गलाने के लिए आवश्यक हो।
- सब्जियों को अधिक भूनना या तलना नहीं चाहिए। तैयार सब्जियों को बार-बार गरम भी नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 10:
भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों ? [2009, 12, 13, 15, 18]
उत्तर:
भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं। अगर किसी प्रकार की गन्दगी उसे बर्तन में लगी हुई हो तो उसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि (UPBoardSolutions.com) भोजन आवश्यकता से अधिक न गल जाए क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे हाथ एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1:
खाद्य सामग्री को क्यों पकाया जाता है? [2011, 13, 14, 15]
या
भोजन पकाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? [2007, 10, 11]
उत्तर:
खाद्य-सामग्री को स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं रोगाणुमुक्त बनाने हेतु तथा विविधता प्रदान करने के लिए पकाया जाता है।
प्रश्न 2:
भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। [2007, 09, 10, 17, 18]
उत्तर:
उबालना, तलना, वाष्प द्वारा पकानां तथा भूनना एवं सेंकना भोजन पकाने की मुख्य विधियाँ हैं।
प्रश्न 3:
भोजन को उबालने से अच्छा भाप द्वारा पकाना होता है क्यों? दो कारण लिखिए।
यो
भोजन पकाने की कौन-सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? [2008]
उत्तर:
भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि उसे भाप द्वारा पकाना होती है। इसके दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं
- भोजन सुपाच्य तथा स्वादिष्ट रहता है।
- भोजन के पोषक तत्त्व नष्ट नहीं होते।

प्रश्न 4:
भोजन को बार-बार गर्म करने से क्या हानि होती है?
उत्तर:
बार-बार गर्म करने से भोजन के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
प्रश्न 5:
धीमी आग पर भोजन पकाने से क्या लाभ हैं?
उत्तर:
धीमी आग पर पकाए गए भोजन के पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं।
प्रश्न 6:
भाप के दबाव से भोजन कैसे पकता है?
उत्तर:
भाप के दबाव के कारण प्रेशर कुकर में उष्णता का घनत्व बढ़ जाने के कारण (UPBoardSolutions.com) भोजन कम समय में ही भली-भाँति पक जाता है।
प्रश्न 7:
भूनने व सेंकने में क्या अन्तर है? [2015, 16, 17]
उत्तर:
भूनते समय भोज्य वस्तु आग के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं आती, जबकि सेंकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेंका जाता है।
प्रश्न 8:
भाप द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ हैं? [2008]
उत्तर:
भाप द्वारा भोजन पकाने से उसके अधिकांश पौष्टिक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं।
प्रश्न 9:
तले हुए भोजन का अधिक सेवन करने से क्या हानि है?
उत्तर:
तला हुआ भोजन गरिष्ठ एवं कुपाच्य होता है। अतः अधिक सेवन करने पर अपच एवं कब्ज़ उत्पन्न करता है।
प्रश्न 10:
दूध को पकाने से क्या लाभ है?
उत्तर:
पकाए जाने पर दूध रोगाणुमुक्त तथा सुपाच्य हो जाता है।
प्रश्न 11:
मक्खन को गर्म करने से क्या हानि सम्भव है?
उत्तर:
गर्म करने पर मक्खन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित विटामिन ‘ए’ नष्ट हो जाता है।
प्रश्न 12:
गृहिणी के लिए हाथ व नाखून स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
हाथ वे नाखूनों की गन्दगी में रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जो कि भोजन पकाते एवं (UPBoardSolutions.com) परोसते समय भोजन में मिल सकते हैं। अत: प्रत्येक गृहिणी को अपने हाथ व नाखून अच्छी तरह साफ रखने चाहिए।

प्रश्न 13:
आलू को बिना छीले पकाने से क्या लाभ हैं?
उत्तर:
आलू के छिलके के कारण उसका विटामिन ‘सी’ सुरक्षित रहता है।
प्रश्न 14:
हरी शाक-सब्जियों को काटने से पूर्व धोना चाहिए। क्यों? [2007, 11, 15, 18]
उत्तर:
यदि सब्जियों को छीलकर एवं काटकर धोया जाता है, तो उनके कुछ विटामिन एवं खनिज-लवण पानी में बह जाते हैं। अतः इन खनिज तत्त्वों की सुरक्षा के लिए सब्जियों को छीलने एवं काटने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए।
प्रश्न 15:
कच्चा भोजन खाने से क्या हानि हो सकती है?
उत्तर:
कच्चा भोजन खाने से खाद्य-पदार्थों के साथ आये हुए रोगों के जीवाणु शरीर में पहुँचेंगे।
प्रश्न 16:
खाद्य-सामग्री को पकाते समय ढककर रखना क्यों आवश्यक होता है?
उत्तर:
खाद्य सामग्री के पोषक तत्त्वों एवं सुगन्ध को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा शीघ्र पकाने के लिए उसे ढककर रखना आवश्यक होता है।
प्रश्न 17:
भोजन पकाने की प्रक्रिया में पौष्टिक तत्त्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए।
उत्तर:
भोजन पकाने की प्रक्रिया में पौष्टिक तत्त्वों की सुरक्षा हेतु उपाय अग्रलिखित हैं
- भोजन पकाते समय बर्तन को खुला न रखें। बर्तन खुला रखने पर भोजन वायु के सम्पर्क में आने से कीटाणु व धूल का प्रवेश होता है।
- भोजन देर तक न पकाएँ। इससे भोजन के पौष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
- आवश्यकता से अधिक मसालों का प्रयोग कदापि न करें।

प्रश्न 18:
गहरी चिकनाई और उथली चिकनाई में तलने की विधियों के बारे में लिखिए। [2007]
उत्तर:
तलने की गहरी चिकनाई विधि:
इस विधि में गहरी कड़ाही प्रयोग में लाई जाती है और काफी मात्रा में घी या तेल में भोज्य-पदार्थ को डालकर तला जाता है; जैसे-पूड़ी-कचौरी, पकौड़ी, समोसे आदि।
तलने की उथली चिकनाई विधि:
इस विधि में चौड़ी व उथली कंड़ाहीं या तवा प्रयोग में लाया जाता है जिसमें (UPBoardSolutions.com) थोड़ी-सी ही चिकनाई डालकर तला जाता है; जैसे—पराँठे, आलू की टिकिया, आमलेट, चीले आदि।
प्रश्न 19:
भोजन परोसने की दो मुख्य शैलियाँ कौन-सी हैं ? [2008, 10]
उत्तर:
भोजन परोसने की दो मुख्य शैलियाँ हैं
- देशी शैली तथा
- विदेशी या परम्परागत शैली।
प्रश्न 20:
जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। [2011]
उत्तर:
जल में घुलनशील विटामिन हैं-विटामिन ‘बी’ कॉम्प्लेक्स, विटामिन ‘सी’ तथा विटामिन ‘पी।
प्रश्न 21:
वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। [2011, 13]
उत्तर:
जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन ‘ए’, विटामिन ‘डी’, विटामिन ‘ई’ तथा विटामिन ‘के’।
प्रश्न 22:
किन-किन फलों में विटामिन ‘सी’ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? [2009, 11]
उत्तर:
समस्त खट्टे फलों अर्थात् नींबू, नारंगी, सन्तरा, अमरूद, अनन्नास तथा तरबूज में विटामिन ‘सी’ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
प्रश्न 23:
कच्ची सब्जियों के खाने से शरीर को कौन-से पोषक तत्त्व अधिक मात्रा में मिलेंगे ? [2009, 13, 15]
उत्तर:
कच्ची सब्जियों के खाने से शरीर को खनिज, विटामिन्स आदि पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 24:
शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? [2015, 17]
उत्तर:
जीवित प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रोगों से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा नियमित रूप से भूख शान्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक है।
प्रश्न 25:
भोजन में कौन-से आवश्यक पोषक तत्त्व पाये जाते हैं? [2015]
या
भोजन के पौष्टिक तत्त्वों के नाम बताइए। [2016]
उत्तर:
भोजन के आवश्यक पोषक तत्त्व हैं–प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, (UPBoardSolutions.com) विटामिन, खनिज तथा जल।
प्रश्न 26:
पौष्टिक भोजन से क्या तात्पर्य है? [2016]
उत्तर:
जो भोजन हमारे शरीर को पुष्ट कर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, पौष्टिक भोजन कहलाता है।
प्रश्न 27:
हमारे शरीर में विटामिन ‘सी’ के दो कार्य लिखिए। [2016]
उत्तर:
1. रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
2. दाँतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न:
निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्पों का चुनाव कीजिए
1. पाक-क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है
(क) अपाच्य
(ख) सुपाच्य (ग) कुपाच्य
(घ) कोई प्रभाव नहीं पड़ता
2. भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है [2015]
(क) उबालना
(ख) भूनना
(ग) तलना
(घ) सिझाना (स्ट्यू करना)
3. दूध को गर्म करने से नष्ट होते हैं [2008]
या
दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाते हैं? [2014, 17]
(क) उसके पोषक तत्त्वे
(ख) उसके कीटाणु
(ग) उसका स्वाद
(घ) कुछ भी नहीं
4. दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है
(क) गर्म करने पर
(ख) ठण्डा करने पर
(ग) उबालने पर
(घ) पानी मिलाने पर
5. सब्जियों को लोहे की कड़ाही में पकाने से
(क) लौह तत्त्व की प्राप्ति होती है।
(ख) विषैलापन आ जाता है।
(ग) स्वाद नष्ट हो जाता है।
(घ) पौष्टिक तत्त्वों की प्राप्ति होती है।

6. डबलरोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है
(क) ग्रिलिंग
(ख) रोस्टिग
(ग) बेकिंग
(घ) टोस्टिंग
7. भोजन को पकाने से नष्ट न होने वाला विटामिन कौन-सा है?
(क) ‘बी’
(ख) ‘सी’
(ग) “के
(घ) ‘ए’
8. सब्जियों को कब धोना चाहिए ?
(क) काटने के बाद
(ख) छीलने के बाद
(ग) छीलने से पहले
(घ) कभी भी
9. सब्जी को बार-बार गर्म करने से नष्ट हो जाता है, उसका
(क) थायमीन
(ख) एस्कॉर्बिक एसिड
(ग) रिबोफ्लेविन
(घ) निकोटिनिक एसिड
10. बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से तरकारियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्त्व है
(क) विटामिन ‘बी’
(ख) प्रोटीन
(ग) कार्बोज
(घ) खनिज-लवण
11. भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? [2007, 16, 18]
(क) घी
(ख) मसाले
(ग) सोडा
(घ) इनमें से किसी को नहीं
12. भोजन परोसने की किस शैली में खड़े-खड़े भोजन किया जाता है?
(क) पाश्चात्य शैली
(ख) भारतीय शैली
(ग) बुफे शैली
(घ) इनमें से कोई नहीं
13. भोजन को स्वास्थ्यवर्द्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए
(क) भोजन को पकाने की
(ख) भोजन को तलने की
(ग) भोजन में पाए जाने वाले तत्त्वों की
(घ) भोजन परोसने की

14. किस प्रकार भोजन पकाने से पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं ? [2009, 10, 15, 18]
(क) उबालकर
(ख) भूनकर
(ग) तलकर
(घ) भाप द्वारा
15. विटामिन ‘डी’ का स्रोत है [2008]
(क) दालें
(ख) सूर्य किरणें
(ग) खट्टे फल
(घ) सब्जियाँ
16. स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? [2008]
(क) विटामिन ‘ए’
(ख) विटामिन ‘डी’
(ग) विटामिन ‘सी’
(घ) विटामिन ‘बी’
17. दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? [2008, 16]
(क) ‘ए’
(ख) ‘डी’
(ग) ‘सी’
(घ) ‘के’
18. विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन-सा रोग हो जाता है ? [2009, 17]
(क) खुजली
(ख) पेचिस
(ग) रतौंधी
(घ) रिकेट्स

19. खट्टे फलों में कौन-सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? [2009, 10, 13, 14]
(क) विटामिन ‘ए’
(ख) विटामिन ‘बी’
(ग) विटामिन ‘सी’
(घ) विटामिन ‘डी’
20. प्रोटीन का मुख्य स्रोत है [2009, 12]
(क) चावल
(ख) चीनी
(ग) दूध
(घ) अंगूर
21. रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है ? [2009, 17]
(क) विटामिन ‘ए’
(ख) विटामिन ‘बी’
(ग) विटामिन ‘सी’ ।
(घ) विटामिन ‘डी’
22. विटामिन का कौन-सा समूह वसा में घुलनशील है ? [2009]
(क) ए, बी, सी, डी
(ख) ए, बी, ई, के
(ग) ए, सी, ई, के
(घ) ए, डी, ई, के
23. भोजन पकाने में समय की बचत होती है [2009]
(क) तलकर
(ख) उबालकर
(ग) प्रेशर कुकरे द्वारा
(घ) भूनकर
24. विटामिन ‘ए’ को उत्तम स्रोत है [2011, 13, 16]
(क) दाल
(ख) दूध
(ग) खट्टे फल
(घ) पीली और हरी सब्जियाँ
25. भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है [2011]
(क) प्रोटीन
(ख) विटामिन
(ग) कार्बोहाइड्रेट
(घ) खनिज लवण
26. लौह तत्त्व की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? [2011, 12, 15 ]
(क) बेरी-बेरी
(ख) एनीमिया
(ग) मरास्मस
(घ) तपेदिक
27. भोजन पकाने की विधि है [2014]
(क) उबालना
(ख) तलनी
(ग) भाप द्वारा
(घ) ये सभी
28. जल में घुलनशील विटामिन हैं [2013, 15, 16, 17]
(क) विटामिन A, B, C
(ख) विटामिन B, C
(ग) विटामिन A, D.
(घ) विटामिन E, K
29. वसा में कौन-सा विटामिन घुलनशील नहीं है? [2013]
(क) विटामिन-ए
(ख) विटामिन-ई
(ग) विटामिन-बी
(घ) विटामिन-के
30. शरीर-निर्माण में सहायक है [2014, 16]
(क) प्रोटीन
(ख) वसा
(ग) विटामिन
(घ) कार्बोहाइड्रेट
31. प्रोटीन पाया जाता है [2012, 14]
(क) मिठाई में
(ख) दालों/सोयाबीन में
(ग) सन्तरा में
(घ) आलू में
32. प्रोटीन का मुख्य कार्य है [2018]
(क) शरीर की वृद्धि तथा विकास
(ख) ऊर्जा प्रदान करना
(ग) अस्थि-निर्माण करना
(घ) हृदय गति सामान्य रखना
33. प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? [2018]
(क) बेरी-बेरी
(ख) एनीमिया
(ग) मरास्मस
(घ) तपेदिक

34. खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए [2013]
(क) राख से
(ख) अपमार्जक से
(ग) पानी से
(घ) साबुन एवं पानी से
35. किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? [2009, 16, 17]
(क) बिस्कुट
(ख) चावल
(ग) ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियाँ
(घ) चीनी
36. सूर्य की रोशनी हमें देती है [2016]
(क) विटामिन ‘सी’
(ख) विटामिन ‘डी’
(ग) विटामिन ‘ए’
(घ) इनमें से कोई नहीं
37. विटामिन ‘सी’ का सबसे अच्छा स्रोत है [2015, 15, 17, 18]
(क) मूंग दाल
(ख) आँवला
(ग) दही
(घ) चावल
38. गाजर, पपीता और आम से मिलता है [2016, 17]
(क) कैल्सियम
(ख) प्रोटीन
(ग) विटामिन ‘ए’
(घ) लौह तत्त्व
39. किसके प्रयोग से तुरन्त ऊर्जा मिलती है? [2016, 17, 18]
(क) विटामिन
(ख) प्रोटीन
(ग) ग्लूकोज
(घ) खनिज लवण
40. खाद्य-पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है [2016]
(क) सुखाकर
(ख) चाशनी में रखकर
(ग) तेल व नमक द्वारा
(घ) इन सभी के द्वारा

उत्तर:
1. (ख) सुपाच्य,
2. (क) उबालना,
3. (ख) उसके कीटाणु,
4. (ग) उबालने पर,
5. (क) लौह तत्व की प्राप्ति होती है,
6. (ग) बेकिंग,
7, (ख) ‘सी’,
8. (ग) छीलने से पहले,
9. (ख) एस्कॉर्बिक एसिड,
10. (क) विटामिन ‘बी’,
11. (ग) सोडा,
12. (ग) बुफे शैली,
13. (ग) भोजन में पाये जाने वाले तत्वों की,
14. (घ) भाप द्वारा,
15. (ख) सूर्य किरणें,
16. (ग) विटामिन ‘सी’,
17. (ग) ‘सी’,
18. (घ) रिकेट्स,
19. (ग) विटामिन ‘सी’,
20. (ग) दूध,
21. (क) विटामिन ‘ए’,
22. (घ) ए, डी, ई, के,
23. (ग) प्रेशर कुकर द्वारा,
24. (ख) दूध,
25. (ग) कार्बोहाइड्रेट,
28 (ख) एनीमिया,
27. (घ) ये सभी,
28. (ख) विटामिन B,C.
29. (ग) विटामिन-बी,
30. (क) प्रोटीन,
31. (ख) दालों/सोयाबीन में,
32. (क) शरीर की वृद्धि तथा विकास,
33. (ग) मरास्मस,
34. (घ) साबुन एवं पानी से,
35. (ग) ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां,
36. (ख) विटामिन डी’,
37. (ख) आँवला,
38. (ग) विटामिन ‘ए’,
39. (ग) ग्लूकोज,
40. (घ) इन सभी के द्वारा।
We hope the UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 15 भोजन पकाना और परोसना तथा तत्त्वों की सुरक्षा help you. If you have any query regarding UP Board Solutions for Class 10 Home Science Chapter 15 भोजन पकाना और परोसना तथा तत्त्वों की सुरक्षा, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
![]()
![]()
![]()


![]()